Haryana State Board HBSE 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 11 भक्तिन Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Hindi Solutions Aroh Chapter 11 भक्तिन
HBSE 12th Class Hindi भक्तिन Textbook Questions and Answers
पाठ के साथ
प्रश्न 1.
भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा?
उत्तर:
भक्तिन का वास्तविक नाम लछमिन अर्थात् लक्ष्मी था। लक्ष्मी धन-संपत्ति की देवी होती है। परंतु इस लक्ष्मी के भाग्य में धन तो नाममात्र भी नहीं था। उसे हमेशा गरीबी भोगनी पड़ी। केवल कुछ दिनों के लिए उसे भरपेट भोजन मिल सका, जब वह अपने पति के साथ परिवार से अलग होकर रहने लगी थी। अन्यथा आजीवन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अतः धन की देवी लक्ष्मी का मान रखने के लिए वह हमेशा अपने नाम को छुपाती रही। उसने केवल लेखिका को अपना सही नाम बताया, परंतु साथ ही यह भी निवेदन कर दिया कि वह उसे लछमिन (लक्ष्मी) नाम से कभी न पुकारे।
भक्तिन को लछमिन (लक्ष्मी) नाम उसके माता-पिता ने दिया होगा। इस नाम के पीछे उनकी स्नेह-भावना रही होगी। शायद उन्होंने यह भी सोचा होगा कि यह नाम रखने से उनके अपने घर में धन का आगमन होगा और विवाह के बाद वह किसी खाते-पीते परिवार में ब्याही जाएगी। अतः उन्होंने अपनी बेटी को लक्ष्मी स्वरूप मानकर उसका यह नाम रखा होगा।
प्रश्न 2.
दो कन्या-रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र-महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अकसर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं?
उत्तर:
भक्तिन ने दो नहीं, अपितु तीन कन्याओं को जन्म दिया था। कन्या-रत्न उत्पन्न करने के बावजूद भक्तिन पुत्र-महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी रही। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय समाज युगों से बेटियों की अपेक्षा बेटों को महत्त्व देता रहा है। भक्तिन की जिठानियाँ यह सोचकर स्वयं को भाग्यवान समझती रहीं और भक्तिन की उपेक्षा करती रहीं। भक्तिन के संदर्भ में यह धारणा सही प्रतीत होती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उपेक्षा तथा घृणा घर की स्त्रियों से ही प्राप्त हुई। उसका पति तो उसे हमेशा सम्मान एवं आदर देता रहा।
सच्चाई तो यह है कि स्त्रियाँ स्वयं ही अपने-आप को पुरुषों से हीन समझती हैं। इसीलिए वे पुत्रवती होने की कामना करती हैं। इसके पीछे समाज की यह धारणा भी चली आ रही है कि बेटे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं, बेटियाँ नहीं। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे भी नारियों की सहमति हमेशा होती है। विशेषकर, सास ही बहू को इस काम के लिए उकसाती है। स्त्रियाँ ही लड़का-लड़की के भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। वे ही दहेज की माँग रखती हैं। यही नहीं, बहू को कष्ट देने में सास की विशेष भूमिका रहती है। अतः यह कहना सर्वथा उचित होगा कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है।

प्रश्न 3.
भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा ज़बरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार (विवाह करें या न करें अथवा किससे करें) इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे?
उत्तर:
भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के तीतरबाज़ साले ने जोर ज़बरदस्ती की, वह निश्चय से रेप था। उसे इस दुराचरण के लिए दंड मिलना चाहिए था। लेकिन गाँव की पंचायत ने न्याय न करके अन्याय किया और लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे तीतरबाज़ युवक की पत्नी घोषित कर दिया। विवाह के मामले में लड़की की रजामंदी की ओर हमारा समाज ध्यान नहीं देता। यह निश्चय से मानवाधिकार का हनन है। विशेषकर, गाँवों की पंचायतें हमेशा लड़कियों के स्वर को दबाने का काम करती रही हैं, जिससे भक्तिन की बेटी के समान कोई भी लड़की विरोध करने का साहस नहीं करती। अतः भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा ज़बरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलना है।
प्रश्न 4.
भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं- लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा?
उत्तर:
लेखिका को पता है कि भक्तिन में अनेक गुणों के बावजूद कुछ दुर्गुण भी हैं। भक्तिन के निम्नलिखित कार्य ही दुर्गुण कहे जा सकते हैं और लेखिका भी ऐसा ही मानती है।
- भक्तिन लेखिका के इधर-उधर पड़े पैसों को भंडार-घर की मटकी में छिपाकर रख देती है। पूछने पर वह इसे चोरी नहीं मानती, बल्कि तर्क देकर इसे पैसे सँभालकर रखना कहती है और लेखिका को ये पैसे लौटाती नहीं।
- जब उसकी मालकिन कभी उस पर क्रोधित होती है तो वह बात को इधर-उधर कर बताती है और इसे झूठ बोलना नहीं मानती।
शास्त्रीय कथनों का वह इच्छानुसार व्याख्या करती है।। - वह दूसरों के कहे को नहीं मानती, बल्कि दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेती है।
- स्वामिनी द्वारा चले जाने के आदेश को वह हँसकर टाल देती है और लेखिका के घर को छोड़कर नहीं जाती।
प्रश्न 5.
भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है?
उत्तर:
भक्तिन स्वयं को बहुत समझदार समझती है। वह प्रत्येक बात का अपने ढंग से अर्थ निकालना जानती है। जब लेखिका ने उसे सिर मुंडवाने से रोकना चाहा तो भक्तिन ने शास्त्रों की दुहाई दी और यह कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है-“तीरथ गए मँडाए सिद्ध”। लगता है यह उक्ति उसकी अपनी गढी हई है अथवा लोगों से सनी-सुनाई है।
प्रश्न 6.
भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गईं?
उत्तर:
भक्तिन स्वयं पूर्णतया देहाती थी। वह अपनी देहाती जीवन-पद्धति को नहीं छोड़ सकी। इसलिए उसने महादेवी को भी अपने साँचे में ढाल लिया। उसे जो कुछ सहज और सरल पकाना आता था, महादेवी को वही खाना पड़ता था। लेखिका को रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ता था। बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़ते थे और ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी भी खानी पड़ती थी। यह सब देहाती भोजन था और यही महादेवी को खाने के लिए मिलता था। अतः महादेवी भी भक्तिन के समान देहाती बन गई।
पाठ के आसपास
प्रश्न 1.
आलो आँधारि की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं?
उत्तर:
बेबी हालदार और भक्तिन दोनों ही नारी जाति के अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। जिस प्रकार बेबी हालदार अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए सभी झुग्गी वालों का विरोध करती है और पति के अभाव में भी मेहनत द्वारा अपने बच्चों को पालती है, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ते हुए अपने जेठ तथा जिठानियों के अन्याय का विरोध करती है। वह निरंतर संघर्ष करके अंत तक अपनी ज़मीन-जायदाद की हकदार बनी रहती है। पुनः ये दोनों नायिकाएँ दूसरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं तथा सादा और सरल जीवन व्यतीत करती हैं।
प्रश्न 2.
भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया, वह आज भी कोई हैरतअंगेज़ बात नहीं है। अखबारों या टी०वी० समाचारों में आनेवाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें।
उत्तर:
आज भी ग्राम पंचायतें रूढ़ियों एवं जड़-परंपराओं का ही पालन कर रही हैं। विशेषकर, बेटियों के मामले में हमारी पंचायतें रूढ़ियाँ ही अपनाती हैं। भले ही गाँव के दबंग लोग निम्न जाति की औरतों अथवा लड़कियों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करें, लेकिन ग्राम पंचायतें उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पातीं। अकसर अखबारों या टी०वी० पर इस प्रकार के समाचार पढ़ने या देखने को मिलते रहते हैं कि एक ही गाँव के युवक-युवती के विवाह को भाईचारे के नाम पर अवैध घोषित किया जाता है और उन्हें भाई-बहन बन कर रहना पड़ता है। जो भी पंचायत के तुगलकी फरमान का उल्लंघन करता है उसका वध तक कर दिया जाता है। अतः विवाह के मामले में हमारी पंचायतों का रुख आज भी रूढ़िवादी है।

प्रश्न 3.
पाँच वर्ष की वय में ब्याही जानेवाली लड़कियों में सिर्फ भक्तिन नहीं है, बल्कि आज भी हज़ारों अभागिनियाँ हैं। बाल-विवाह और उम्र के अनमेलपन वाले विवाह की अपने आस-पास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें।
उत्तर:
निम्नलिखित बिंदुओं पर विद्यार्थी अपने मित्रों के साथ परिचर्चा कर सकते हैं
- भले ही हमारे देश में बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन कानूनों का उल्लंघन होता रहता है।
- राजस्थान में एक विशेष पर्व के अवसर पर हज़ारों की संख्या में बाल-विवाह होते हैं।
- गाँवों में तो बाल-विवाह की बात आम है, परंतु शहरों में भी इस प्रकार के विवाह होते रहते हैं।
- लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर लोगों को बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराना आवश्यक है।
प्रश्न 4.
महादेवी जी इस पाठ में हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूलि आदि के माध्यम से पशु-पक्षी को मानवीय वाली लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु-पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर रेखाचित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूँढ़कर पढ़ें। जो मेरा परिवार नाम से प्रकाशित है।
उत्तर:
पुस्तकालय से ‘मेरा परिवार’ गद्य रचना को लेकर विद्यार्थी स्वयं पढ़ें। इस गद्य रचना में गिल्लू, सोना, नीलकंठ, गोरा, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूलि के बारे में विस्तार से पढ़ा जा सकता है।
भाषा की बात
प्रश्न 1.
नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा-प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ-छवि स्पष्ट कीजिए
(क) पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले
(ख) खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी
(ग) अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण
उत्तर:
अर्थ-छवि:
(क) प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि भक्तिन ने उसी प्रकार पहली कन्या के बाद दो अन्य कन्याओं को जन्म दिया, जैसे किसी पुस्तक के नए संस्करण प्रकाशित होते हैं।
(ख) टकसाल में सिक्के ढालने का काम होता है, परंतु हमारे समाज में लड़के को खरा सिक्का और लड़की को खोटा सिक्का माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पराया धन होती है तथा उसके विवाह में दान-दहेज देना पड़ता है। यहाँ भक्तिन द्वारा एक-एक करके तीन लड़कियों को जन्म देने के कारण व्यंग्य रूप से उसे खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी कहा गया है।
(ग) वस्तुतः भक्तिन अपने पिता की बीमारी का पता करने के लिए अपने मायके गई तो उस समय गाँव की औरतों द्वारा फुसफुसाते हुए यह बात बार-बार कही गई ‘वो आई, लक्ष्मी आ गई’। औरतों की इस फुसफुसाहट में भक्तिन के प्रति स्पष्ट सहानुभूति प्रकट की जा रही थी। क्योंकि उसकी विमाता ने बीमारी के दौरान ज़मीन-जायदाद के चक्कर में उसे सूचना नहीं भेजी थी।
प्रश्न 2.
‘बहनोई’ शब्द ‘बहन (स्त्री.) + ओई’ से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अनन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुंलिंग शब्दों में कुछ स्त्री-प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द में कुछ पुं. प्रत्यय जोड़कर पुंलिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पुं. प्रत्यय ‘ओई’ हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसे कुछ और शब्द और उनमें लगे पुं. प्रत्ययों की हिंदी तथा और भाषाओं में खोज करें।
उत्तर:
ननद शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें ‘ओई’ (पुं. प्रत्यय) जोड़कर ‘ननदोई’ शब्द बनाया जाता है। जिसका अर्थ है- ननद का पति। विद्यार्थी शब्दकोश की सहायता से पुं. प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त करें।
प्रश्न 3.
पाठ में आए लोकभाषा के इन संवादों को समझ कर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढाल कर प्रस्तुत कीजिए।
(क) ई कउन बड़ी बात आय। रोटी बनाय जानित है, दाल राँध लेइत है, साग-भाजी /उक सकित है, अउर बाकी का रहा।
(ख) हमारे मालकिन तौ रात-दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं। अब हमहूँ पढ़े लागब तो घर-गिरिस्ती कउन देखी-सुनी।
(ग) ऊ बिचरिअउ तौ रात-दिन काम माँ झुकी रहती हैं, अउर तुम पचै घूमती-फिरती हौ, चलौ तनिक हाथ बटाय लेउ।
(घ) तब ऊ कुच्छौ करिहैं धरि ना-बस गली-गली गाउत-बजाउत फिरिहैं।
(ङ) तुम पचै का का बताईयहै पचास बरिस से संग रहित है।
(च) हम कुकुरी बिलारी न होय, हमार मन पुसाई तौ हम दूसरा के जाब नाहिं त तुम्हार पचै की छाती पै होरहा पूँजब और राज करब, समुझे रहो।।
उत्तर:
(क) यह कौन-सी बड़ी बात है। रोटी बनाना जानती हूँ, दाल राँध (पका) लेती हूँ, साग-सब्जी छौंक सकती हूँ और बाकी क्या रहा।
(ख) हमारी मालकिन तो रात-दिन पुस्तकों में लगी रहती है। अब यदि मैं भी पढ़ने लग गई तो घर-गृहस्थी को कौन देखेगा।
(ग) वह बेचारी तो रात-दिन काम में लगी रहती है और तुम लोग घूमते-फिरते हो। जाओ, थोड़ा उनकी सहायता करो।
(घ) तब वह कुछ करता-धरता नहीं है, बस गली-गली में गाता-बजाता फिरता है।
(ङ) तुम लोगों को क्या बताऊँ पचास वर्षों से साथ रह रही हूँ।
(च) मैं कोई कुत्तिया या बिल्ली नहीं हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊँगी, नहीं तो तुम्हारी छाती पर बैठकर अनाज भूगूंगी और राज करूँगी, यह बात अच्छी तरह से समझ लो।

प्रश्न 4.
भक्तिन पाठ में पहली कन्या के दो संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका के खास भाषाई संस्कार की पहचान कराता है, साथ ही ये प्रयोग कथ्य को संप्रेषणीय बनाने में भी मददगार हैं। वर्तमान हिंदी में भी कुछ अन्य प्रकार की शब्दावली समाहित हुई है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिससे वक्ता की खास पसंद का पता चलता है। आप वाक्य पढ़कर बताएँ कि इनमें किन तीन विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है? इन शब्दावलियों या इनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप भी कुछ वाक्य बनाएँ और कक्षा में चर्चा करें कि ऐसे प्रयोग भाषा की समृद्धि में कहाँ तक सहायक है?
→ अरे! उससे सावधान रहना! वह नीचे से ऊपर तक वायरस से भरा हुआ है। जिस सिस्टम में जाता है उसे हैंग कर देता है।
→ घबरा मत! मेरी इनस्वींगर के सामने उसके सारे वायरस घुटने टेकेंगे। अगर ज़्यादा फाउल मारा तो रेड कार्ड दिखा के हमेशा के लिए पवेलियन भेज दूंगा।
→ जानी टेंसन नई लेने का वो जिस स्कूल में पढ़ता है अपुन उसका हैडमास्टर है।
उत्तर:
उपर्युक्त वाक्यों में कंप्यूटर, खेल जगत तथा मुंबई फिल्मी दुनिया की शब्दावली का प्रयोग देखा जा सकता है।
(i) वायरस, सिस्टम तथा हैंग तीनों ही कंप्यूटर-प्रणाली के शब्द हैं। इनके अर्थ हैं-
- वायरस – दोष
- सिस्टम – प्रणाली
- हैंग – ठहराव
अथवा गतिरोध या बाधा इस वाक्य का अर्थ होगा कि अरे भाई उस व्यक्ति से खबरदार रहना, वह पूर्णतया दोषों से ग्रस्त है। जिसके यहाँ भी जाता है, वहाँ पर वह सारी व्यवस्था को खराब कर देता है।।
(ii) इनस्वींगर, फाउल, रेड कार्ड तथा पवेलियन, ये चारों शब्द क्रिकेट खेल जगत से संबंधित हैं।
इनस्वींगर – भीतर तक भेदने की कोशिश करना।
- फाउल – दोषपूर्ण कार्य
- रेड कार्ड – बाहर जाने का इशारा
- पवेलियन – वापिस घर भेजना, बाहर कर देना।
इस वाक्य का अर्थ होगा कि घबरा मत! मैं इस प्रकार का कार्य करूँगा कि उसे भीतर तक चोट लगेगी और उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। यदि उसने अधिक गड़बड़ी की तो मैं बच्चू को ऐसी कानूनी कार्रवाई में फँसाऊँगा कि वह यहाँ से बाहर हो जाएगा।
(iii) जानी! (संबोधन), टेंसन, स्कूल, हैडमास्टर ये चारों शब्द मुंबई फिल्मी जगत के हैं।
- जानी – हल्का-फुल्का संबोधन
- टेसन – चिंता करना
- स्कूल में पढ़ना – काम करना
- हैडमास्टर होना – बढ़-चढ़ कर होना, उस्तादों का उस्ताद होना।
इस वाक्य का अर्थ होगा कि प्रिय मित्र! तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। वह जो कुछ भी कर रहा है, मैं उस काम का अच्छा जानकार हूँ। सब कुछ ठीक कर दूंगा।
HBSE 12th Class Hindi भक्तिन Important Questions and Answers
प्रश्न 1.
भक्तिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
भक्तिन महादेवी की प्रमुख सेविका थी। वह महादेवी की आयु से लगभग पच्चीस वर्ष बड़ी थी। इसलिए वह स्वयं को लेखिका की अभिभाविका समझती थी। उसकी सेवा-भावना में अभिभाविका जैसा अधिकार था, परंतु उसके हृदय में माँ की ममता भी थी। यद्यपि गृहस्थ जीवन में भक्तिन को अधिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन महादेवी के यहाँ रहते हुए उसे सुखद जीवन प्राप्त हुआ। भले ही वह स्वभाव से कर्कश तथा दुराग्रही थी। परंतु महादेवी के प्रति उसमें आदर-सम्मान तथा समर्पण की भावना थी। वह अपनी स्वामिन को सबसे महान मानती थी। उसने लेखिका की भलाई चाहने के लिए उसकी रुचि तथा आदतों में परिवर्तन कर दिया।
वह छाया के समान महादेवी के साथ लगी रहती थी, भले ही महादेवी के कुत्ते-बिल्ली तक सो जाते थे, परंतु भक्तिन तब तक नहीं सोती थी, जब तक उसकी मालकिन जागती रहती थी। जहाँ आवश्यकता पड़ती, वह तत्काल सहायता के लिए पहुँच जाती थी। यद्यपि भक्तिन युद्ध तथा जेल जाने से बहुत डरती थी, परंतु अपनी मालकिन के लिए वह जेल जाने को भी तैयार थी। जब नगर भर में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो भी भक्तिन ने अपनी मालकिन का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए भक्तिन ने जल्दी ही एक सच्ची अभिभाविका का पद प्राप्त कर लिया। इसके साथ-साथ भक्तिन संस्कारवान, परिश्रमी तथा मधुर स्वभाव की नारी भी थी। यही कारण है कि उसका पति उससे अत्यधिक प्रेम करता था।
प्रश्न 2.
भक्तिन का नामकरण किसने किया और क्यों?
उत्तर:
भक्तिन का असली नाम लछमिन (लक्ष्मी) था, परंतु महादेवी की सेवा करते हुए वह अपना मूल नाम छिपाना चाहती थी। क्योंकि यह नाम उसके जीवन के सर्वथा प्रतिकूल था। भक्तिन के हाव-भाव, चाल-चलन, घुटा हुआ सिर और कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका यह नामकरण किया।

प्रश्न 3.
भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दीजिए।
उत्तर:
भक्तिन ऐतिहासिक गाँव झूसी के एक प्रसिद्ध शूरवीर अहीर की इकलौती पुत्री थी। उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे विमाता की देखरेख में आरंभिक जीवन व्यतीत करना पड़ा। पाँच वर्ष की आयु में उसका विवाह हँडिया गाँव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे बेटे के साथ हो गया। नौ वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया। उसके पिता का बेटी के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण विमाता ने उसकी बीमारी का समाचार उसके पास नहीं भेजा।
प्रश्न 4.
भक्तिन के ससुराल वाले उसकी उपेक्षा क्यों करते थे?
उत्तर:
पहली बात तो यह है कि भक्तिन सबसे छोटी बहू थी। इसलिए घर की सास और जिठानियाँ उसे दबाकर रखना चाहती थीं। दूसरा, भक्तिन ने एक के बाद एक तीन बेटियों को जन्म दिया। परंतु सास तथा जिठानियों ने केवल बेटों को जन्म दिया था। इसलिए लड़कियों को जन्म दिए जाने के कारण भक्तिन के ससुराल वाले उसकी उपेक्षा करते थे।
प्रश्न 5.
भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के-लड़कियों में भेदभाव क्यों किया जाता है स्पष्ट करें।
उत्तर:
भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी लड़का-लड़की में भेदभाव किया जाता है। गाँव के लोग लड़के को सोने का खरा सिक्का और लड़कियों को खोटा सिक्का कहते हैं। यही नहीं, लड़की को पराया धन भी कहा जाता है। लड़कियों को जन्म देने के कारण भक्तिन की ससुराल में उपेक्षा की गई और घर के सारे काम करवाए गए। परंतु घर के काले-कलूटे तथा निकम्में पुत्रों को जन्म देने वाली जिठानियाँ अपने पतियों से पिटकर भी घर में आराम करती थीं। उनके काले-कलूटे लड़कों को खाने में राब और मलाई मिलती थी और भक्तिन और उसकी लड़कियों को घर का सारा काम करने के बावजूद भी खाने में काले गुड़ की डली के साथ चना-बाजरा चबाने को मिलता था। आज भी हमारे भारतीय ग्रामीण समाज में अधिकांश लड़कियों को घर के काम-काज तक ही सीमित रखा जाता है और उन्हें उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती।
प्रश्न 6.
महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बाँटा है? प्रत्येक का उल्लेख करें।
उत्तर:
महादेवी ने भक्तिन के जीवन को चार परिच्छेदों में व्यक्त किया है। प्रथम परिच्छेद भक्तिन के विवाह-पूर्व जीवन से संबंधित है। द्वितीय परिच्छेद ससुराल में सधवा के रूप से संबंधित है। तृतीय परिच्छेद का संबंध उसके वैधव्य तथा विरक्त जीवन से है। चतुर्थ परिच्छेद का संबंध उसके उस जीवनकाल से है, जिसमें वह महादेवी की सेवा करती है।
प्रश्न 7.
पति की मृत्यु के बाद ससुराल वाले उसका पुनर्विवाह क्यों करना चाहते थे?
उत्तर:
भक्तिन उनतीस वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। उसने अपनी मेहनत द्वारा अपने खेत और बाग हरे-भरे कर लिए थे। उसके पास दुधारू गाय और भैंस थी। उसके जेठ तथा जिठौत यह चाहते थे कि यदि भक्तिन का दूसरा विवाह हो जाएगा तो उसके घर तथा खेत-खलिहान पर उनका अधिकार स्थापित हो जाएगा। लेकिन भक्तिन उनके मंतव्य को अच्छी प्रकार समझ गई थी और उसने पुनर्विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
प्रश्न 8.
क्या ससुराल से अलग होकर भक्तिन ने सही किया?
उत्तर:
ग्रामीण संस्कृति की दृष्टि से भक्तिन का संयुक्त परिवार से अलग होना अनुचित कहा जा सकता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह बिल्कुल सही है। ससुराल वालों ने भक्तिन को हर प्रकार से दबाया, अपमानित किया और उपेक्षित किया। सास और जिठानियों ने भक्तिन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उसकी बेटियों को भी चना-बाजरा खाकर गुजारा करना पड़ता था। इसलिए भक्तिन ने ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर अपना अलग घर बसाया। हालात को देखते हुए भक्तिन का यह निर्णय सर्वथा उचित कहा जाएगा।

प्रश्न 9.
भक्तिन को बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी क्यों कहा गया है?
उत्तर:
भक्तिन झूसी गाँव के एक शूरवीर अहीर की इकलौती बेटी थी। पिता ने ही उसका नाम लछमिन (लक्ष्मी) रखा था। पाँच वर्ष की अल्पायु में ही उसका विवाह कर दिया गया और नौ वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया। परंतु विमाता ने भक्तिन के पिता की मरणांतक बीमारी की सूचना नहीं दी। यहाँ तक कि संपत्ति की रक्षा के लिए विमाता ने उसके पिता की मृत्यु की बात को छिपाकर रखा। परंतु जब नैहर पहुँचकर भक्तिन को यह सब पता चला तो वह बड़े बाप की बेटी का सारा वैभव ठुकराकर एक चूंट पानी पिए बिना वापिस ससुराल लौट आई थी। यही कारण है कि उसे बड़े बाप वाली बेटी कहा गया है।
प्रश्न 10.
भक्तिन ने अपने वैधव्य को किस प्रकार व्यतीत करने का फैसला किया?
उत्तर:
भक्तिन अपने शूरवीर पिता की इकलौती पुत्री थी। उसमें अच्छे संस्कार भी थे। उसका पति भी उससे अत्यधिक प्रेम करता था। अतः उसने पति की यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। उसने यह भी सोच लिया कि वह सांसारिक मोह-माया से नाता तोड़कर अपनी गृहस्थी चलाएगी। अतः उसने शास्त्र की मर्यादानुसार अपने केश मुंडवा लिए।
प्रश्न 11.
‘भक्तिन’ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हमारे समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है?
उत्तर:
इस पाठ से स्पष्ट है कि हमारा समाज विधवा को अपना शिकार मानता है। आज भी हमारे समाज में विधवा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। चाहे कोई उसका अपना हो या पराया। कोई भी उसे आदर-सम्मान न जेठ-जिठानियाँ तो उसे घर की संपत्ति से वंचित करना चाहते हैं। भक्तिन की बेटी जब विधवा हो गई, तब जेठ के लड़के ने अपने तीतरबाज़ साले को उस विधवा के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उसकी संपत्ति को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार के घृणित कार्य में स्त्रियाँ भी पुरुषों का साथ देती हुई देखी गई हैं। यहाँ तक कि गाँव की पंचायतें भी विधवा की लाज की रक्षा नहीं करतीं। वे भी विधवाओं के लिए बेड़ियाँ तैयार करती हैं। ऐसी स्थिति में विधवाओं का सम्मानजनक पुनर्विवाह ही उचित होगा।
प्रश्न 12.
इस पाठ के आधार पर पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
इस पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि गाँव की पंचायतें गूंगी, अयोग्य तथा लाचार हैं। पंचायत के सभी सदस्य न्याय के आधार नहीं हैं। वे हमेशा शक्तिशाली का पक्ष लेते हैं। उनका न्याय केवल मज़ाक बनकर रह गया है। हमारी पंचायतें कलयुग की दुहाई देकर अत्याचारी की रक्षा करती हैं और पीड़ित व्यक्ति पर अत्याचार करती हैं। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ कुछ ऐसा ही किया गया। भक्तिन की इच्छा के विरुद्ध पंचायत ने उसकी बेटी का विवाह उस तीतरबाज़ युवक से करने की घोषणा की कि जो कुछ भी काम-धाम नहीं करता था। यह तो मानों रावण के साथ सीता का विवाह करने वाली बात हो गई।
प्रश्न 13.
तीन कन्याओं को जन्म देने के बाद भी भक्तिन पुत्र की इच्छा में अंधी अपनी जिठानियों की घृणा तथा उपेक्षा की पात्र बनी रही। इस प्रकार के उदाहरण भारतीय समाज में अभी भी देखने को मिलते हैं। इसका कारण तथा समाधान प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर:
कारण-आज भी भारतीय समाज इस समस्या से ग्रस्त है। प्रायः लोग बेटी की अपेक्षा बेटे को अधिक महत्त्व देते हैं। लोग समझते हैं कि पुत्र कमाऊ होता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। यही कारण है कि समाज में पुरुष को नारी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली माना जाता है। विशेषकर, ग्रामीण समाज में कन्याओं को दबाकर रखा जाता है और उन्हें उचित शिक्षा भी नहीं दी जाती।
समाधान-यदि लड़कियों को उचित शिक्षा दी जाए और उन्हें नौकरी करने तथा व्यवसाय करने के अवसर प्रदान किए जाएँ तो इस समस्या का कुछ सीमा तक हल निकाला जा सकता है। मध्यवर्गीय परिवारों में यह प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ती जा रही है कि बेटे तो अपनी बहुओं को लेकर अपने माँ-बाप से अलग हो जाते हैं, लेकिन बेटियाँ अंत तक अपने माता-पिता का साथ निभा सकती हैं। हमें लड़के-लड़की को ईश्वर की संतान मानकर उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
प्रश्न 14.
भोजन के बारे में भक्तिन का क्या दृष्टिकोण था?
उत्तर:
भक्तिन एक ठेठ ग्रामीण नारी थी। वह सीधा-सादा भोजन ही पसंद करती थी। रसोई की पवित्रता पर वह विशेष ध्यान देती थी। इसलिए उसने महादेवी के घर आकर नहा-धोकर, स्वच्छ साड़ी पर जल छिड़क कर उसे धारण किया और रसोई में मोटे कोयले से रेखा खींचकर भोजन बनाया। उसे गर्व था कि वह साधारण और सरल भोजन बना सकती है। अतः वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके द्वारा पकाए भोजन का तिरस्कार करे।
प्रश्न 15.
पति की मृत्यु के बाद भक्तिन के सामने कौन-कौन सी समस्याएँ पैदा हुईं?
उत्तर:
पति की मृत्यु के पश्चात भक्तिन के समक्ष कछ भयंकर समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। अभी उसकी दो छोटी बेटियाँ कुँवारी बैठी थीं। दूसरा, सगे-संबंधी उसकी घर-संपत्ति पर आँखें गड़ाए बैठे थे। वे लोग चाहते थे कि भक्तिन दूसरा विवाह कर ले, ताकि उसकी संपत्ति उन्हें मिल जाए। परंतु भक्तिन ने इन मुसीबतों का डट कर सामना किया और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ संभाल लिया। तत्पश्चात् भक्तिन की बड़ी बेटी भी विधवा हो गई जिसके फलस्वरूप उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ा।
प्रश्न 16.
किस घटना के फलस्वरूप भक्तिन को घर छोड़कर महादेवी के यहाँ नौकरी करनी पड़ी?
उत्तर:
जैसे-तैसे भक्तिन ने मेहनत करके अपने खेत-खलिहान, अमराई तथा गाय-भैंसों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। उसने अपनी छोटी बेटियों का विवाह भी कर दिया और समझदारी दिखाते हुए बड़े दामाद को घर-जमाई बना लिया। परंतु दुर्भाग्य तो उसके पीछे लगा हुआ था। अचानक उसका दामाद गुजर गया। जिठौतों ने चाल चलकर बलपूर्वक अपने तीतरबाज़ साले को भक्तिन की विधवा बेटी के गले मड़ दिया। जिससे दिन-भर घर में कलह-क्लेश रहने लगा। धीरे-धीरे सारी धन-संपत्ति नष्ट होने लगी। लगान न देने के दंड के रूप में ज़मींदार ने भक्तिन को दिन-भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता पर कलंक के समान था। अतः अगले दिन ही वह काम की तलाश में महादेवी के यहाँ पहुँच गई।

प्रश्न 17.
“इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे जाग्रत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएँ छिपाने लगी।” महादेवी ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है?
उत्तर:
महादेवी ने यह कथन भक्तिन के संदर्भ में कहा है। भक्तिन एक तर्कशील नारी थी और अपनी बात को सही सिद्ध थी। भक्तिन केवल पेट की भूख को शांत करने के लिए सीधा-सादा खाना बनाती थी। धीरे-धीरे महादेवी उसकी इस प्रवृत्ति से प्रभावित होने लगी। वह भी जीवन की सहजता और सरलता के प्रति आकर्षित हो गई और उसने अपनी असुविधाओं को छिपाना आरंभ कर दिया।
प्रश्न 18.
युद्ध के खतरे के बावजूद भक्तिन अपने गाँव क्यों नहीं लौटी?
उत्तर:
युद्ध के खतरे में भी भक्तिन अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और महादेवी के साथ रहना उचित समझा। उसने महादेवी से यह प्रार्थना की कि युद्ध के खतरे को टालने के लिए वह उसके गाँव में चल पड़े। वहाँ पर भी पढ़ने-लिखने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी।
प्रश्न 19.
भक्तिन ने त्याग का कौन-सा उदाहरण प्रस्तुत किया?
उत्तर:
भक्तिन स्वभाव से बड़ी कंजूस औरत थी और एक-एक पाई पर अपनी जान देती थी। परंतु उसके त्याग की पराकाष्ठा उस समय देखी जा सकती है, जब उसने पाई-पाई करके जोड़ी हुई धन-राशि 105 रुपये महादेवी की सेवा में अर्पित कर दिए।
प्रश्न 20.
भक्तिन के मन में जेल के प्रति क्या भाव थे और उसने भय पर किस प्रकार विजय प्राप्त की?
उत्तर:
भक्तिन जेल का नाम सुनते ही काँप उठती थी। उसे लगता था कि ऊँची-ऊँची दीवारों में कैदियों को अनेक कष्ट दिए जाते हैं। परंतु जब उसे पता चला कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए विद्यार्थी भी कारागार में जा रहे हैं और उसकी स्वामिन को भी जेल जाना पड़ सकता है तो उसका भय दूर हो गया और वह भी अपनी स्वामिन के साथ जेल जाने को तैयार हो गई।
प्रश्न 21.
“भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं।” महादेवी के इस कथन का क्या आशय है? .
उत्तर:
भक्तिन को अच्छी सेविका कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। सत्य-असत्य के बारे में उसका अपना दृष्टिकोण था। उसका यह दृष्टिकोण लोक-व्यवहार पर खरा नहीं उतर सकता। इसलिए लेखिका भक्तिन को अच्छी नहीं कह सकती।
प्रश्न 22.
भक्तिन जीवन भर अपरिवर्तित रही-इसका क्या कारण है?
उत्तर:
भक्तिन अपनी आस्था और आदतों की पक्की थी। वह अपनी जीवन-पद्धति को ही सही मानती थी। अडिग रहकर वह अपने तौर-तरीके अपनाती रही। उसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया और न ही शहरी शिष्टाचार को अपनाया। उसने ‘आँय’ कहने आदत को कभी भी ‘जी’ में नहीं बदला। उसने महादेवी को ग्रामीण परिवेश में बदल दिया, परंतु स्वयं नहीं बदली।
बहविकल्पीय प्रश्नोत्तर
1. भक्तिन’ पाठ की रचयिता हैं-
(A) जैनेंद्र कुमार
(B) महादेवी वर्मा
(C) सुभद्रा कुमारी चौहान
(D) रांगेय राघव
उत्तर:
(B) महादेवी वर्मा
2. ‘भक्तिन’ पाठ किस रचना में संकलित है?
(A) स्मृति की रेखाएँ
(B) अतीत के चलचित्र
(C) पथ के साथी
(D) मेरा परिवार
उत्तर:
(A) स्मृति की रेखाएँ
3. भक्तिन किस विधा की रचना है?
(A) निबंध
(B) कहानी
(C) संस्मरणात्मक रेखाचित्र
(D) आलोचना
उत्तर:
(C) संस्मरणात्मक रेखाचित्र
4. महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ?
(A) 1906 में
(B) 1908 में
(C) 1905 में
(D) 1907 में
उत्तर:
(D) 1907 में

5. महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ?
(A) मध्य प्रदेश
(B) उत्तर प्रदेश
(C) राजस्थान
(D) दिल्ली
उत्तर:
(B) उत्तर प्रदेश
6. महादेवी का जन्म किस नगर में हुआ?
(A) फर्रुखाबाद
(B) इलाहाबाद
(C) कानपुर
(D) लखनऊ
उत्तर:
(A) फर्रुखाबाद
7. कितनी आयु में महादेवी का विवाह हुआ?
(A) सात वर्ष में
(B) आठ वर्ष में
(C) नौ वर्ष में
(D) बारह वर्ष में
उत्तर:
(C) नौ वर्ष में
8. महादेवी वर्मा ने किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की?
(A) अंग्रेज़ी
(B) हिंदी
(C) इतिहास
(D) संस्कृत
उत्तर:
(D) संस्कृत
9. महादेवी वर्मा ने किस विश्वविद्यालय से एम०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की?
(A) इलाहाबाद विश्वविद्यालय
(B) कानपुर विश्वविद्यालय
(C) बनारस विश्वविद्यालय
(D) आगरा विश्वविद्यालय
उत्तर:
(A) इलाहाबाद विश्वविद्यालय
10. महादेवी को किस शिक्षण संस्थान की प्रधानाचार्या नियुक्त किया गया?
(A) संस्कृत महाविद्यालय
(B) एस०डी० महाविद्यालय
(C) प्रयाग महिला विद्यापीठ
(D) वनस्थली विद्यापीठ
उत्तर:
(C) प्रयाग महिला विद्यापीठ
11. भारत सरकार ने महादेवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया?
(A) वीरचक्र
(B) शौर्यचक्र
(C) पद्मश्री
(D) पद्मभूषण
उत्तर:
(D) पद्मभूषण
12. किन विश्वविद्यालयों ने महादेवी को डी० लिट्० की मानद उपाधि से विभूषित किया?
(A) पंजाब विश्वविद्यालय तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
(B) विक्रम, कुमायूँ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय
(C) आगरा विश्वविद्यालय तथा कानपुर विश्वविद्यालय
(D) मेरठ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय
उत्तर:
(B) विक्रम, कुमायूँ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय

13. महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ?
(A) 12 सितंबर, 1986
(B) 11 दिसंबर, 1987
(C) 12 जनवरी, 1985
(D) 11 नवंबर, 1988
उत्तर:
(B) 11 दिसंबर, 1987
14. ‘अतीत के चलचित्र’ किसकी रचना है?
(A) महादेवी वर्मा की
(B) सुभद्राकुमारी चौहान की
(C) जयशंकर प्रसाद की
(D) मुक्तिबोध की
उत्तर:
(A) महादेवी वर्मा की
15. ‘श्रृंखला की कड़ियाँ’ किस विधा की रचना है?
(A) काव्य संग्रह
(B) निबंध संग्रह
(C) कहानी संग्रह
(D) रेखाचित्र संग्रह
उत्तर:
(B) निबंध संग्रह
16. ‘स्मृति की रेखाएँ’ की रचयिता है
(A) महादेवी वर्मा
(B) रांगेय राघव
(C) हरिवंशराय बच्चन
(D) रघुवीर सहाय
उत्तर:
(A) महादेवी वर्मा
17. ‘पथ के साथी’ किसकी रचना है?
(A) जैनेंद्र कुमार
(B) धर्मवीर भारती
(C) फणीश्वरनाथ रेणु
(D) महादेवी वर्मा
उत्तर:
(D) महादेवी वर्मा
18. भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी?
(A) हाँसी।
(B) झाँसी
(C) झूसी
(D) अँझूसी
उत्तर:
(C) झूसी
19. भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी?
(A) पंद्रह वर्ष
(B) पच्चीस वर्ष
(C) तीस वर्ष
(D) बीस वर्ष
उत्तर:
(B) पच्चीस वर्ष
20. भक्तिन के सेवा-धर्म में किस प्रकार का अधिकार है?
(A) अभिभाविका जैसा
(B) स्वामी जैसा
(C) सेविका जैसा
(D) माँ जैसा
उत्तर:
(A) अभिभाविका जैसा
21. भक्तिन का स्वभाव कैसा है?
(A) कोमल और मधुर
(B) कर्कश और कठोर
(C) अभिमानी और क्रूर
(D) छल-कपट से पूर्ण
उत्तर:
(B) कर्कश और कठोर

22. भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी?
(A) छाया के समान
(B) धूप के समान
(C) वायु के समान
(D) पालतु पशु के समान
उत्तर:
(A) छाया के समान
23. भक्तिन का शूरवीर पिता किस गाँव का रहने वाला था?
(A) मूंसी
(B) लूसी
(C) झूसी
(D) हँडिया
उत्तर:
(C) झूसी
24. भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था?
(A) भक्तिन
(B) लछमिन (लक्ष्मी)
(C) दासिन
(D) पार्वती
उत्तर:
(B) लछमिन (लक्ष्मी)
25. महादेवी वर्मा क्या पढ़ते-पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अन्तर पर विचार किया करती थीं?
(A) पतंजलि सूत्र
(B) शाल्व सूत्र
(C) ज्ञान सूत्र
(D) न्याय सूत्र
उत्तर:
(D) न्याय सूत्र
26. भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ?
(A) सात वर्ष
(B) आठ वर्ष
(C) चार वर्ष
(D) पाँच वर्ष
उत्तर:
(D) पाँच वर्ष
27. भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ?
(A) नौ वर्ष
(B) बारह वर्ष
(C) तेरह वर्ष
(D) दस वर्ष
उत्तर:
(A) नौ वर्ष
28. लेखिका के द्वारा पुकारी जाने पर भक्तिन क्या कहती थी?
(A) जी
(B) आई मालकिन
(C) आँय
(D) हाँ, जी
उत्तर:
(C) आँय
29. महादेवी को ‘यामा’ पर कौन-सा पुरस्कार प्राप्त हुआ?
(A) शिखर सम्मान
(B) साहित्य अकादमी पुरस्कार
(C) ज्ञानपीठ पुरस्कार
(D) पहल सम्मान
उत्तर:
(C) ज्ञानपीठ पुरस्कार
30. उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी को कौन-सा पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया?
(A) भारत भारती पुरस्कार
(B) राहुल पुरस्कार
(C) प्रेमचंद पुरस्कार
(D) शिखर पुरस्कार
उत्तर:
(A) भारत भारती पुरस्कार

31. महादेवी वर्मा को पद्मभूषण की उपाधि कब मिली?
(A) 1958 में
(B) 1957 में
(C) 1956 में
(D) 1960 में
उत्तर:
(C) 1956 में
32. भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी-
(A) ओठों के कोनों में
(B) छोटी आँखों में
(C) विश्वास भरे कंठ में
(D) ऊँची आवाज़ में
उत्तर:
(B) छोटी आँखों में
33. ‘कृषीवल’ शब्द का क्या अर्थ है?
(A) किसान
(B) मजदूर
(C) बैल
(D) अन्न
उत्तर:
(C) बैल
34. ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किसने किया?
(A) जिठानियों ने
(B) पति ने
(C) सास ने
(D) ससुर ने
उत्तर:
(B) पति ने
35. भक्तिन के ओंठ कैसे थे?
(A) पतले
(B) मोटे
(C) कटे-फटे
(D) अवर्णनीय
उत्तर:
(A) पतले
36. भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा?
(A) ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके
(B) ताकि वे भक्तिन की घर-संपत्ति को हथिया सकें
(C) ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सकें
(D) ताकि वे भक्तिन को पुनः समाज में सम्मान दे सकें
उत्तर:
(B) ताकि वे भक्तिन की घर-संपत्ति को हथिया सकें
37. हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है?
(A) स्नेहपूर्ण
(B) असम्मानपूर्ण
(C) सहानुभूतिपूर्ण
(D) सम्मानपूर्ण
उत्तर:
(B) असम्मानपूर्ण
38. भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है?
(A) पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं।
(B) वे सही न्याय नहीं कर पाती
(C) वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं
(D) वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं
उत्तर:
(A) पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं
39. सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी?
(A) शबरी
(B) सुग्रीव
(C) हनुमान
(D) लक्ष्मण
उत्तर:
(C) हनुमान
40. भक्तिन का शरीर कैसा था?
(A) मोटा
(B) दुबला
(C) लम्बा
(D) दिव्य
उत्तर:
(B) दुबला

41. खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ क्या है?
(A) निकम्मे काम करने वाली पत्नी
(B) बेकार पत्नी
(C) जिस टकसाल से खोटे सिक्के निकलते हैं
(D) कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी
उत्तर:
(D) कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी
42. महादेवी ने लछमिन को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया?
(A) उसके व्यवहार को देखकर
(B) उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर
(C) उसके गले में कंठी माला देखकर
(D) उसकी शांत मुद्रा को देखकर
उत्तर:
(C) उसके गले में कंठी माला देखकर
43. भक्तिन क्या नहीं बन सकी?
(A) गोरखनाथ
(B) एकनाथ
(C) सत्यवादी हरिश्चन्द्र
(D) मीराबाई
उत्तर:
(C) सत्यवादी हरिश्चन्द्र
44. भक्तिन किससे डरती थी?
(A) बादल से
(B) हिरन से
(C) कारागार से
(D) संसार से
उत्तर:
(C) कारागार से
45. भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी?
(A) उन्नीस
(B) पच्चीस
(C) उनतीस
(D) तीस
उत्तर:
(C) उनतीस
भक्तिन प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या
[1] सेवक-धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या
गोपालिका की कन्या है-नाम है लछमिन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बँध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने-अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है; पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि-सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया; पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूँ। [पृष्ठ-71]
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व पर बहुत ही रोचक प्रकाश डाला है। इसमें लेखिका भक्तिन की तुलना रामभक्त हनुमान से करती हैं।
व्याख्या-लेखिका ने भक्तिन की कर्मठता एवं उनके प्रति लगाव तथा सेविका-धर्म की तुलना अंजनी-पुत्र महावीर हनुमान जी से की है। लेखिका कहती है कि सेवक-धर्म में रामभक्त हनुमान जी रामायण के एक महान पात्र हैं। भक्तिन सेवक-धर्म में उनका मुकाबला करने वाली एक नारी थी। वह किसी अंजना की बेटी न होकर एक संज्ञाहीन, परंतु धन्य माँ गोपालिका की बेटी थी। उसका नाम लछमिन अथवा लक्ष्मी था। भले ही वह एक अहीरन की पुत्री थी, परंतु वह बहुत ही कर्मनिष्ठ थी। लेखिका स्पष्ट करती है कि जिस प्रकार मेरे नाम का विस्तार मेरे लिए धारण न करने योग्य है, उसी प्रकार भक्तिन के मस्तक की सिकुड़ी रेखाओं में लक्ष्मी का धन-वैभव रुक नहीं पाया। भाव यह है कि भले ही मेरा नाम महादेवी है, परंतु मैं देवी के गुणों को धारण नहीं कर सकती।
उसी नाम भले ही लक्ष्मी था, परंतु उसके पास कोई धन-संपत्ति नहीं थी। नाम के गुण प्रायः लोगों में नहीं होते। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को अपने नाम से विपरीत परिस्थितियों में जीवन-यापन करना पड़ता है; जैसे लोग नाम रख लेते हैं करोड़ीमल, परंतु उस करोड़ीमल के पास दो वक्त का भोजन नहीं होता। लेकिन भक्तिन बड़ी समझदार थी, इसलिए वह धन-संपत्ति को सूचित करने वाला नाम किसी को नहीं बताती थी। परंतु जब वह नौकरी खोजते-खोजते मेरे पास आई थी, तब उसने बड़ी ईमानदारी से अपना परिचय दिया। अपनी संपूर्ण जीवन-गाथा का विवरण देते हुए उसने यह भी बता दिया कि उसका मूल नाम लक्ष्मी है, परंतु साथ ही उसने मुझसे यह भी निवेदन कर दिया कि मैं कभी भी उसके इस नाम का प्रयोग न करूँ।
विशेष-
- इस गद्यांश में लेखिका ने भक्तिन के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी सेवा-भक्ति की तुलना हनुमान जी की सेवा-भक्ति के साथ की है।
- भक्तिन का नाम भले ही लक्ष्मी था, परंतु यह नाम उसकी गरीबी का मज़ाक उड़ाता था। इसलिए वह अपने इस नाम को छिपाने का प्रयास करती थी।
- सहज, सरल तथा संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा का सफल प्रयोग किया गया है।
- वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है तथा वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है। m गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए।
(ख) हनुमान जी और भक्तिन में क्या समानता थी?
(ग) लेखिका ने अपने नाम को दुर्वह क्यों कहा है?
(घ) भक्तिन अपने मूल नाम को छिपाना क्यों चाहती थी?
(ङ) ‘कपाल की कुंचित रेखाओं से क्या भाव है?
(च) अपने-अपने नाम के विरोधाभास का क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
(क) पाठ का नाम-भक्तिन लेखिका का नाम-महादेवी वर्मा।
(ख) हनुमान जी और भक्तिन दोनों ही सच्चे सेवक होने के साथ-साथ भक्त भी थे। दोनों अपने-अपने स्वामी की सच्चे मन से सेवा करते रहे। जिस तरह से हनुमान ने राम की सेवा और भक्ति की, उसी प्रकार भक्तिन भी महादेवी की सेवा करती रही।
(ग) लेखिका का नाम महादेवी है। परंतु वे स्वीकार करती हैं कि वे चाहते हुए भी महादेवी का पद प्राप्त नहीं कर पाई। इसी कारण लेखिका ने अपने नाम को दुर्वह कहा।
(घ) भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था लक्ष्मी अर्थात् धन-वैभव की देवी परंतु भक्तिन बहुत गरीब थी। यह नाम उसकी गरीबी का मज़ाक उड़ा. रहा था। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी को यह पता चले कि उसका नाम लक्ष्मी है। इसलिए वह अपने नाम को छिपाती रही।
(ङ) ‘कपाल की कुंचित रेखाओं का भाव है भाग्य की रेखाओं का बहुत छोटा होना। लेखिका यह स्पष्ट करना चाहती है कि भक्तिन का भाग्य खोटा था। उसे जीवन-भर सुख-समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी।
(च) अपने-अपने नाम का विरोधाभास से अभिप्राय है कि नाम के विपरीत जीवन का होना। प्रायः सभी लोगों को अपने-अपने नाम के विपरीत जीना पड़ता है। उदाहरण के रूप में किसी महिला का नाम सरस्वती होता है, परंतु वह एक अक्षर भी पढ़ना नहीं जानती। जैसे किसी पुरुष का नाम लखपतराय होता है, पर उसके पास न रहने को घर होता है और न ही खाने को दो वक्त का भोजन होता है। इसका एक ही कारण है कि हमारे नाम हमारे गुणों के अनुसार नहीं होते। इसीलिए सभी के नामों में विरोधाभास होता है।

[2] पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा, जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने-पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना-उढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गाँव की सीमा में पहुँचते ही झड़ गए। ‘हाय लछमिन अब आई’ की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गईं। पर वहाँ न पिता का चिह्न शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उलटे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी-खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक-फेंककर उसने पिता के चिर विछोह की मर्मव्यथा व्यक्त की। [पृष्ठ-72]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ में संकलित है। इसमें लेखिका भक्तिन के पिता के देहांत तथा उसकी विमाता के दुर्व्यवहार पर प्रकाश डालती है। लेखिका कहती है
व्याख्या-पिता के प्रति भक्तिन के मन में अत्यधिक प्रेमभाव था, परंतु उसकी विमाता न केवल उससे ईर्ष्या करती थी, बल्कि अपनी संपत्ति में से उसे कुछ भी देना नहीं चाहती थी। इसलिए विमाता ने उसके पिता के प्राणांतक रोग का समाचार भक्तिन के पास नहीं भेजा। जब उसकी मौत हो गई, तब ही उसे यह समाचार भेजा गया। इधर सास ने भी उसे उसके पिता की मृत्यु की खबर नहीं दी। वह नहीं चाहती थी कि भक्तिन यहीं पर रोना-पीटना शुरू कर दे, बल्कि यह कह दिया कि वह काफी दिनों से अपने मायके नहीं गई है, इसलिए उसे वहाँ जाकर सबसे मिल कर आना चाहिए। यह कहकर भक्तिन की सास ने उसे खूब सजा-पहनाकर मायके भेजा। भक्तिन को इस कृपा की आशा नहीं थी। परंतु जब उसे बैठे-बिठाए मायके जाने की अनुमति मिल गई, तब वह तीव्र गति से अपने मायके की ओर बढ़ने लगी। परंतु गाँव में घुसते ही उसकी गति तब मंद पड़ गई, जब लोग उसे देखकर कहने लगे कि बहुत दुख हुआ लछमिन तू इतने दिनों के बाद आई।
‘हाय लछमिन अब आई’। उसे ये शब्द बार-बार सुनने पड़े और लोगों की सहानुभूति लेनी पड़ी। जैसे-तैसे वह अपने घर पहुंची। वहाँ उसके पिता का कोई नामो-निशान नहीं था अर्थात् वह मर चुका था। विमाता का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा नहीं था। इस दुख से थकी-माँदी तथा अपमान की आग में जलती हुई उसने अपने मायके से एक गिलास पानी तक भी नहीं पिया। वह ज्यों-की-त्यों तत्काल अपने ससुराल वापिस आ गई। घर आते ही उसने सास को खूब भला-बुरा कहा और अपनी विमाता पर आए हुए क्रोध को शांत किया। यही नहीं, उसने अपने गहने उतारकर पति पर फेंक-फेंककर मारे और पिता से जीवन भर के वियोग की असहनीय पीड़ा को व्यक्त किया। भाव यह है कि भक्तिन के साथ उसकी विमाता और सास दोनों ने भारी धोखा किया। न तो विमाता ने यह सूचना भेजी कि उसका पिता मृत्यु देने वाले रोग से ग्रस्त है और न ही सास ने उसे सूचित किया कि उसके पिता का देहांत हो गया है।
विशेष-
- यहाँ लेखिका ने भक्तिन के पिता की घातक बीमारी और उनकी मृत्यु का संवेदनशील वर्णन किया है।
- भक्तिन को अपनी सास और विमाता दोनों से तिरस्कार और धोखा मिला।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा विषयानुकूल है तथा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) भक्तिन की विमाता ने उसके पिता के मरणांतक रोग का समाचार क्यों नहीं भेजा?
(ख) भक्तिन की सास ने पहना-उढ़ाकर उसे नैहर क्यों भेजा?
(ग) सास के अनुग्रह को लेखिका ने अप्रत्याशित क्यों कहा है?
(घ) गाँव पहुंचते ही भक्तिन की आशा के पंख झड़ क्यों गए?
(ङ) भक्तिन ने किस प्रकार अपने पिता की मृत्यु के शोक को व्यक्त किया?
उत्तर:
(क) भक्तिन के पिता उसे अगाध प्रेम करते थे। इसी कारण विमाता भक्तिन से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके मन में यह भी डर था कि अपने पिता के प्राणांतक अर्थात् मृत्यु देने वाले रोग को देखकर कहीं वह उसके घर में धन-संपत्ति का झगड़ा न खड़ा कर दे। इसलिए उसने भक्तिन को उसके पिता की भयानक बीमारी का समाचार नहीं भेजा।
(ख) भक्तिन की सास मृत्यु के विलाप को अपशकुन मानती थी। वह नहीं चाहती थी कि भक्तिन अपने पिता की मृत्यु के समाचार को पाकर घर में रोना-धोना शुरू कर दे और आस-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाएँ। इसलिए उसकी सास ने उसको यह कहकर मायके भेजा कि वह बहुत दिनों से अपने पिता के घर नहीं गई है। अतः वह जाकर उन्हें देख आए।
(ग) सास का भक्तिन को उसके मायके भेजना उसकी आशा के सर्वथा विपरीत था। भक्तिन को इस बात की आशा नहीं थी कि उसकी सास उसे माता-पिता से मिलने के लिए मायके भेज देगी। इसीलिए सास का यह आग्रह अप्रत्याशित ही कहा जाएगा।
(घ) जैसे ही भक्तिन अपने गाँव में पहुँची तो लोग उसे देखकर बड़ी सहानुभूति के साथ कहने लगे-‘हाय, लछमिन अब आई। लोगों की हाय को सुनकर भक्तिन का दिल बैठने लगा और उसके मन में आशा के जो पँख फड़फड़ाए थे, वह तत्काल झड़ गए।
(ङ) भक्तिन ने अपनी सास को खरी-खोटी बातें सुनाकर और अपने गहने उतारकर अपने पति पर फेंक-फेंककर अपने पितृ-शोक को व्यक्त किया।
[3] जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुँए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास तीन-तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियाँ काक-भुशंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। [पृष्ठ-72]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के गृहस्थ जीवन पर समुचित प्रकाश डाला है। लेखिका कहती है
व्याख्या-पिता की मृत्यु के बाद जहाँ उसे अपने मायके में दुख प्राप्त हुआ, वहीं अपने गृहस्थी जीवन में भी उसको सुख की बजाय दुख ही अधिक प्राप्त हुआ। उसकी पहली संतान एक लड़की थी, जो गेहुँए रंग की थी। इसके पश्चात् उसने दो और कन्याओं को जन्म दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सास तथा जिठानियाँ उसकी उपेक्षा करने लगी। उस समय के हालात में यह सही भी था। कारण यह था कि भक्तिन की सास तीन बेटों को जन्म देकर घर की मुखिया बन चुकी थी। उसके तीनों बेटे कमाने वाले थे। दूसरी ओर, दोनों जिठानियों ने कौए जैसे काले पुत्रों को जन्म दिया और वे दोनों घर के मुखिया पद की दावेदार बन गईं। भक्तिन सबसे छोटी बहू थी। उसने अपनी सास तथा जिठानियों की परंपरा का पालन नहीं किया अर्थात् उसने बेटों को जन्म न देकर तीन बेटियों को जन्म दिया। इसलिए उसे उपेक्षा का दंड भोगना पड़ा। कहने का भाव यह है कि परिवार में भक्तिन की उपेक्षा इसलिए की जा रही थी, क्योंकि उसने बेटों की बजाय बेटियों को जन्म दिया था।
विशेष-
- इसमें लेखिका ने भक्तिन के वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डाला है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उस समय के समाज में लड़के की माँ होना सम्माननीय माना जाता था।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और भावानुकूल है।
- वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हए भक्तिन की व्यथा पर प्रकाश डाला गया है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) इस गद्यांश में जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या अभिप्राय है?
(ख) सास और जिठानियों ने भक्तिन की उपेक्षा करनी क्यों आरंभ कर दी?
(ग) लेखिका द्वारा सास का भक्तिन की उपेक्षा करना उचित क्यों ठहराया गया है?
(घ) इस गद्यांश से नारी मनोविज्ञान का कौन-सा रहस्य प्रकट होता है?
(ङ) भारतीय परिवारों में सम्मानीय पुरखिन का पद किसे मिलता है?
उत्तर:
(क) जीवन के दूसरे परिच्छेद से अभिप्राय है-भक्तिन के वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन का आरंभ होना । लेखिका की दृष्टि में यह भक्तिन के जीवन का दूसरा अध्याय है।
(ख) भक्तिन ने एक के बाद एक तीन बेटियों को जन्म दिया, जबकि उसकी सास और जिठानियों ने बेटों को जन्म दिया था। इसीलिए सास और जिठानियाँ उसकी उपेक्षा करने लगी थीं।
(ग) वस्तुतः लेखिका का यह कथन व्यंग्यात्मक है। यहाँ लेखिका ने समाज की इस रूढ़ि पर कठोर प्रहार किया है। भारतीय समाज में लड़के की माँ होना सम्मानजनक माना जाता है और लड़की के जन्म को अशुभ कहा जाता है। भक्तिन की सास ने एक के बाद एक तीन बेटों को जन्म दिया था तो वह तीन बेटियों को जन्म देने वाली भक्तिन की उपेक्षा क्यों न करती? इसीलिए लेखिका ने उसे उचित ठहराया है।
(घ) इस गद्यांश में लेखिका ने नारी-मनोविज्ञान के इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि नारी ही नारी की दुश्मन होती है। कुछ नारियाँ अपनी जिठानियों, देवरानियों, सासों और बहुओं के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रच देती हैं कि सीधी-सादी नारी का जीना भी कठिन हो जाता है। यहाँ भक्तिन को घर की नारियों की उपेक्षा को सहन करना पड़ा। इस पाठ में लेखिका ने इस नारी-मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है कि प्रायः नारी ही पुत्र को जन्म देकर खुश होती है और पुत्री के जन्म पर शोक मनाने लगती है। परंतु धीरे-धीरे अब यह धारणा समाप्त होती जा रही है।
(ङ) भारतीय परिवारों में सम्माननीय पुरखिन का पद केवल उसी नारी को प्राप्त होता है जो कमाऊ पुत्रों को जन्म देती है, बेटियों को नहीं।
[4] इस दंड-विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी, जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल-जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली-चबाई की परिणति, उसके पत्नी-प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात-बात पर धमाधम पीटी-कूटी जाती; पर उसके पति ने उसे कभी उँगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम-रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अँगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय-भैंस, खेत-खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। [पृष्ठ-72-73]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि घर-परिवार में भले ही भक्तिन की उपेक्षा होती थी, परंतु उसक का पति उससे अत्यधिक प्यार करता था।
व्याख्या-संयुक्त परिवारों में बेटियों को जन्म देने वाली नारियों को उपेक्षा का दंड भोगना पड़ता है। लेकिन इस दंड-व्यवस्था कोई नियम नहीं था, जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल अर्थात कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी को उसके पति से अलग किया जा सके। भक्तिन की सास तथा जिठानियाँ प्रायः भक्तिन के पति के सामने उसकी चुगली करती रहती थीं। वे चाहती थीं कि उसका पति उसकी पिटाई करे। लेकिन इन चुगलियों का प्रभाव उल्टा हुआ और पति उससे और अधिक प्रेम करने लगा। दूसरी ओर, जिठानियों की छोटी-छोटी बातों पर पिटाई होती थी। जबकि भक्तिन के पति ने कभी उसे मारा नहीं था। वह इस बात को जानता था कि भक्तिन बड़े बाप की बेटी है और उसमें अच्छे संस्कार भी हैं। इसके साथ-साथ भक्तिन बड़ी मेहनती, तेजस्विनी और अपने पति के प्रति समर्पित नारी थी। अपने पति के प्रेम के बल पर ही उसने संयुक्त परिवार से अलग होकर अपनी अलग घर-गृहस्थी बसाकर अपनी जिठानियों को अँगूठा दिखा दिया। चूँकि घर का सारा काम भक्तिन ही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेल-खलिहान एवं आम के पेड़ों के बारे में उसका ज्ञान सबसे अधिक था।
विशेष-
- यहाँ लेखिका ने भक्तिन के पति-प्रेम का यथार्थ वर्णन किया है। भक्तिन ने अपने मधुर स्वभाव, अच्छे संस्कार और कार्य-कुशलता से पति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित व भावानुकूल है।
- वर्णनात्मक शैली द्वारा भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) ‘खोटे सिक्कों की टकसाल’ से क्या अभिप्राय है?
(ख) घर-भर में उपेक्षित होकर भी भक्तिन सौभाग्यशालिनी क्यों थी?
(ग) ‘चगली-चबाई की परिणति पत्नी-प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी’-इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए।
(घ) भक्तिन के किन गुणों के कारण उसका पति उससे प्रेम करता था?
(ङ) भक्तिन ने क्या करके ईर्ष्यालु जिठानियों को अँगूठा दिखा दिया? ।
उत्तर:
(क) लेखिका ने भक्तिन के लिए ही खोटे सिक्कों की टकसाल का प्रयोग किया है, क्योंकि उसने एक के बाद एक तीन बेटियों को जन्म दिया था। परंतु लेखिका के इस कथन में समाज पर करारा व्यंग्य है जो कन्याओं को ‘खोटा सिक्का’ मानता है और कन्याओं की माताओं को अपमानित करता है।
(ख) भक्तिन के ससुराल में सास तथा जिठानियाँ हमेशा उसकी उपेक्षा करती थीं। जिठानियाँ तो काले-कलूटे बेटों को जन्म देकर घर में आराम से बैठती थीं और भक्तिन को घर का सारा काम करना पड़ता था। फिर भी वह बहुत सौभाग्यशालिनी थी, क्योंकि उसकी जिठानियाँ अपने पतियों के द्वारा धमाधम पीटी जाती थी, परंतु उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। उसने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था।
(ग) भक्तिन की सास तथा जिठानियाँ अकसर भक्तिन के पति से उसकी चुगलियाँ करती रहती थीं। वे चाहती थीं कि जैसे वे अपने पतियों द्वारा धमाधम पीटी जाती हैं, उसी प्रकार भक्तिन की भी पिटाई होनी चाहिए। परंतु उनकी चुगलियों का प्रभाव उल्टा ही पड़ा और भक्तिन का पति उससे और अधिक प्रेम करने लगा।
(घ) भक्तिन के मधुर स्वभाव, अच्छे संस्कार, मेहनत, तेज तथा कार्य-कुशलता के कारण उसका पति उससे अत्यधिक प्रेम करता था।
(ङ) भक्तिन अपनी ईर्ष्यालु जिठानियों की उपेक्षा से तंग आ चुकी थी। अतः उसने अपने पति-प्रेम के बल पर अपने परिवार से अलग होकर अपनी घर-गृहस्थी बसा ली। उसने उनको यह दिखा दिया कि यदि वे उसकी उपेक्षा करती रहेंगी तो वह भी उन्हें अपने जीवन से अलग कर सकती है।
[5] भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, इसी से किशोरी से युक्ती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भइयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ-का-तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ-बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देख-भाल करने लगी और ‘मान न मान मैं तेरा मेहमान’ की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी-न-किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। [पृष्ठ-73-74]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने गाँव की एक अभावग्रस्त तथा गरीब भक्तिन का यथार्थ संस्मरणात्मक रेखाचित्र अंकित किया है। लेखिका भक्तिन के दुर्भाग्य पर प्रकाश डालती हुई लिखती है कि
व्याख्या – भक्तिन का दुर्भाग्य उससे भी अधिक हठी था। वह जितना भी दुर्भाग्य से लड़ती, उतना ही दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ता जाता। यही कारण है कि किशोरावस्था से यौवनावस्था में कदम रखते ही भक्तिन की बड़ी बेटी के पति का देहांत हो गया और वह विधवा हो गई। उसके जेठ अपनी भाभी पर तो कोई नियंत्रण नहीं पा सके थे, परंतु उसकी बेटी के विधवा होने के कारण जेठों और उनके पुत्रों में आशा की एक किरण जाग गई। परिणाम यह हुआ कि विधवा बहन के पुनर्विवाह के लिए जेठ का बड़ा लड़का अपने उस साले को गाँव में ले आया, जो तीतर लड़ाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं करता था।
बड़े जिठौत को यह लगा कि यदि उनकी विधवा बहन उसके साले की पत्नी बन जाएगी तो सारी संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाएगा, लेकिन भक्तिन की बेटी अपनी माँ से अधिक समझदार निकली। वह सारी बात को अच्छी प्रकार समझ गई। उसने तीतर लड़ाने वाले वर को अस्वीकार कर दिया। दूसरे चचेरे भाइयों के लिए बाहर से किसी व्यक्ति का बहनोई बनकर आना उनके लिए कोई सुखद नहीं था। उनका विधवा बहन के विवाह का प्रस्ताव ज्यों-का-त्यों रह गया अर्थात् जिठौत के साले का प्रस्ताव लगभग समाप्त हो गया। माँ-बेटी दोनों मिलकर खूब परिश्रम करके अपनी संपत्ति की अच्छी तरह से देखभाल करने लगी।
परंतु तीतर लड़ाने वाले साले का समर्थन करने वाले जेठ के पुत्र ‘मान न मान, मैं तेरा मेहमान’ कहावत को सिद्ध करना चाहते थे अर्थात् वे बलपूर्वक विधवा बहन का किसी-न-किसी तरह विवाह करना चाहते थे। इसके लिए वे नए-नए उपाय खोजने लगे। कहने का भाव है कि जिठौतों ने यह फैसला कर लिया कि वे किसी-न-किसी तरह भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह उस तीतर लड़ाने वाले से अवश्य करेंगे, ताकि वे भक्तिन की संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर सकें।

विशेष-
- यहाँ लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि भक्तिन के जेठ उसकी घर-संपत्ति पर किसी-न-किसी तरह अधिकार करना चाहते थे। इसलिए वे अपनी इच्छानुसार भक्तिन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह कराना चाहते थे।
- सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।
- वर्णनात्मक शैली का सफल प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित और सटीक है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) भक्तिन का दुर्भाग्य किससे अधिक हठी था और क्यों था?
(ख) जेठ भइयहू से पार क्यों नहीं पा रहे थे? उनका मंतव्य क्या था?
(ग) भक्तिन के जिठौतों को आशा की कौन-सी किरण दिखाई दी?
(घ) बड़ा जिठौत अपने साले के साथ भक्तिन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह क्यों करना चाहता था?
(ङ) भक्तिन की विधवा बेटी ने क्या समझदारी दिखाई?
उत्तर:
(क) भक्तिन का दुर्भाग्य भक्तिन से भी अधिक हठी था। विधवा होने के बाद भक्तिन ने अपने सिर के बाल भी मुंडवा लिए थे। वह बड़ी दृढ़ता के साथ इस प्रतिज्ञा का पालन कर रही थी। परंतु उसका दुर्भाग्य भक्तिन की इस प्रतिज्ञा से अधिक कठोर निकला। भक्तिन के बड़े दामाद का निधन हो गया और उसकी बेटी यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही विधवा हो गई।
(ख) भक्तिन के जेठों की यह इच्छा थी कि भक्तिन की ज़मीन-जायदाद पर उनका अधिकार हो जाए। इसीलिए वे भक्तिन की बड़ी विधवा लड़की का पुनर्विवाह करना चाहते थे।
(ग) जब भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा हो गई तो जेठ के लड़कों को लगा कि अब वे भक्तिन की ज़मीन-जायदाद पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी चचेरी बहन का पुनर्विवाह कराने का फैसला कर लिया। उनके लिए यह एक सबसे अच्छा उपाय था।
(घ) बड़ा जिठौत अपने साले के साथ भक्तिन की विधवा बेटी का पुनर्विवाह इसलिए करना चाहता था, ताकि वह भक्तिन की घर संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त कर सके।
(ङ) भक्तिन की बड़ी लड़की बहुत समझदार थी। वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसके चचेरे भाई उनकी ज़मीन-जायदाद पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। यदि उसका विवाह तीतरबाज़ वर के साथ हो गया तो उसके चचेरे भाइयों को उसकी घर-संपत्ति पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए समझदारी दिखाते हुए उसने इस रिश्ते को ठुकरा दिया।
[6] तीतरबाज़ युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी पाँचों उँगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध-का-दूध पानी-का-पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला-हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलियुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे पर जब वे एक कोठरी से निकले, तब उनका पति-पत्नी के रूप में रहना ही कलियुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से सँभाले हुए गाय-ढोर, खेती-बारी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर ज़मींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया, अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुँची। [पृष्ठ-74]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ में संकलित है। इसमें लेखिका ने गाँव की एक अभावग्रस्त तथा गरीब भक्तिन के कष्टों का वर्णन किया है। इसमें लेखिका ने उस प्रसंग को उठाया है जब बड़े जिगत का तीतरबाज साला विधवा बेटी के कमरे में बलपूर्वक घुस गया था और यह मामला पंचायत के सामने रखा गया। इस संदर्भ में लेखिका पंचायत के अन्यायपूर्ण निर्णय पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि-
व्याख्या-तीतरबाज़ युवक ने पंचायत के सामने अपनी सफाई में कहा कि वह युवती का निमंत्रण पाकर ही उसकी कोठरी में गया था, परंतु युवती ने उसके इस कथन का विरोध करते हुए कहा कि तीतरबाज़ युवक के मुख पर उसकी पाँचों उँगलियों के उभरे निशान यह स्पष्ट करते हैं कि उसका दावा गलत है और वह बलपूर्वक उसकी कोठरी में घुस आया था। इसमें उसकी सहमति नहीं थी। आखिर सही न्याय करने के लिए पंचायत बिठाई गई। पंचायत के सभी सदस्यों ने सिर हिलाकर यह स्वीकार किया कि कलयुग ही इस समस्या का मूल कारण है। पंचायत ने एक ऐसा निर्णय किया, जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती थी। पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन दोनों में से चाहे एक सच्चा व्यक्ति हो, चाहे दोनों झूठे व्यक्ति हों, परंतु जब वे दोनों एक ही कोठरी से बाहर निकलकर आए हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को पति-पत्नी बनकर रहना पड़ेगा।
केवल यही हल ही कलयुग के इस दोष का निराकरण कर सकता है। इसके सिवाय अब कोई उपाय नहीं है। अन्ततः जिस लड़की का गाँव भर में अपमान हुआ था, वह अपने दाँतों से होंठ काटकर रह गई और भक्तिन ने भी क्रोधित दृष्टि से बलपूर्वक बने हुए उस दामाद को देखा और अपने क्रोध को अंदर-ही-अंदर पी लिया। यह रिश्ता भी अधिक सुखद नहीं हुआ। क्योंकि भक्तिन का दामाद अब बेफिक्र होकर तीतर लड़ाने लगा। बेटी मजबूर होकर क्रोध की आग में जलती रहती थी।
भक्तिन और उसकी बेटी ने बड़ी कोशिश करके अपने घर के पशुओं तथा खेती-बाड़ी को सँभाल रखा था, परंतु अब पारिवारिक झगड़ों में सब कुछ जल कर खत्म हो गया। सुखपूर्वक रहने की तो बात ही समाप्त हो गई। यहाँ तक कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। जब भक्तिन लगान अदा नहीं कर सकी तो ज़मींदार ने भक्तिन को अपने यहाँ बुलाकर दिन-भर कड़ी धूप में खड़ा रहने का दंड दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। वह एक कर्त्तव्यपरायण नारी थी और यह दंड उसके लिए कलंक के समान सिद्ध हुआ। अगले ही दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर नगर में आ गई। भाव यह है कि तीतरबाज के साथ भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह हो जाने पर उसकी सारी संपत्ति बरबाद हो गई।
विशेष-
- इसमें लेखिका ने जहाँ एक ओर गाँव की पंचायत के अन्याय पर प्रकाश डाला है, वहीं दूसरी ओर भक्तिन की जमीन-जायदाद की बर्बादी के कारणों का भी ब्यौरा दिया है।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है।
- वर्णनात्मक शैली द्वारा लेखिका ने भक्तिन की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है।
- वाक्य-विन्यास बहुत ही सटीक एवं विषयानुकूल है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) युवती ने पंचायत के सामने क्या तर्क दिया और पंचायत ने क्या फैसला लिया?
(ख) आपकी दृष्टि में क्या पंचायत का फैसला उचित है?
(ग) ज़बरदस्ती शादी कराने में कौन दोषी है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
(घ) ज़बरदस्ती शादी कराने का क्या दुष्परिणाम हुआ?
(ङ) भक्तिन को काम करने के लिए शहर क्यों आना पड़ा?
उत्तर:
(क) युवती ने पंचायत के सामने कहा कि यह युवक उसकी कोठरी में बलपूर्वक घुस आया है। मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ मारकर उसका विरोध किया और उसकी पिटाई भी की। यही कारण है कि मेरी पाँचों उँगलियों के निशान उसके गालों पर उभरे हुए हैं। पंचायत ने यह फैसला लिया कि भक्तिन की विधवा लड़की और जिठौत के साले के बीच जो घटना घटी है उसके लिए कलयुग ही दोषी है, क्योंकि दोनों एक ही कमरे में बंद हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें पति-पत्नी बनकर ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार पंचायत के सदस्यों ने जबरदस्ती उन दोनों का विवाह करवा दिया।
(ख) पंचायत का फैसला अन्यायपूर्ण है। लेखिका ने इसके लिए ‘अपीलहीन’ शब्द का प्रयोग किया है जो यह सिद्ध करता है कि पंचायत का फैसला एक तरफा था। उन्होंने सच-झूठ का पता नहीं लगाया और लड़की के न चाहते हुए भी उस गुंडे तीतरबाज़ के साथ उसका विवाह करा दिया। किसी भी दृष्टि से यह फैसला उचित नहीं कहा जा सकता।
(ग) भक्तिन की विधवा लड़की का पुनर्विवाह कराने के लिए पंचायत ही दोषी है। भक्तिन के जिठौत तो संपत्ति को हथियाने के चक्कर में था और उसके साले ने लोभ और पागलपन में यह दुष्कर्म किया। परंतु पंचायत का काम न्याय करना होता है। उसे मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय करना चाहिए था। पंचायत का यह कर्त्तव्य था कि वह उस तीतरबाज़ को अपमानित करके उसे गाँव से निकाल देती, ताकि कोई व्यक्ति गाँव की बहू-बेटी के साथ दुष्कर्म न करे। इसके साथ-साथ जिठौत को भी दंड दिया जाना चाहिए था।
(घ) भक्तिन की विधवा बेटी की जबरदस्ती शादी कराने का यह दुष्परिणाम हुआ कि उसकी हरी-भरी गृहस्थी उजड़ गई। अनचाहे निकम्मे दामाद के कारण निरंतर कलह बढ़ने लगा, जिससे खेती-बाड़ी पर प्रभाव पड़ा। तीतरबाज़ दामाद ने घर की संपत्ति को उजाड़कर रख दिया। जिससे भक्तिन के पास लगान चुकाने के पैसे भी नहीं रहे। अन्ततः जमींदार से अपमानित होने के कारण भक्तिन ने कमाई के लिए शहर का रुख किया।
(ङ) भक्तिन को कमाई के लिए शहर इसलिए आना पड़ा, क्योंकि उसके दामाद तथा जिठौतों के दुष्कर्मों के कारण उसकी हरी-भरी खेती उजड़ गई थी। उसके पशु और खेत उसकी कमाई का साधन न रहकर बोझ बन गए थे।
[7] दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली थोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का, दो लोटे जल से अभिनंदन किया। दो मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक-विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक-कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत-पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात-बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। [पृष्ठ-74-75]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है, जब वह लेखिका के पास आकर नौकरी करना आरंभ करती है।
व्याख्या-अगले दिन सवेरा होते ही भक्तिन ने अपने सिर पर कई लोटे पानी उँडेलकर स्नान किया। तत्पश्चात् लेखिका की धुली धोती को पानी के छींटे मारकर पवित्र करके पहन लिया। पूर्व दिशा के अंधकार से सूर्योदय हो रहा था और लेखिका के घर की दीवार से पीपल का एक पेड़ फूट कर निकल आया था। भक्तिन ने दो लोटे जल चढ़ाकर सूर्य और पीपल का स्वागत किया। ने दो मिनट तक अपनी नाक को दबाकर रखा तथा जाप किया। इसके पश्चात उसने कोयले की मोटी रेखा खींचकर अपने क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित कर दिया। इस प्रकार वह रसोई घर में प्रविष्ट हुई। यह सब देखकर लेखिका को समझने में तनिक भी देर नहीं हुई कि इस सेविका के साथ गुजारा करना बड़ा कठिन है।
लेखिका पुनः स्वीकार करती है कि भोजन के संबंध में वह पूर्णतया विरक्त है, फिर भी अपने परिवार में वह पाक-विद्या में निपुण मानी जाती है। जो व्यक्ति पाक-विद्या में निपुण होता है, वह दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन में नुक्ताचीनी अवश्य करता है और लेखिका भी कोई अपवाद नहीं थी। परंतु जब लेखिका ने छूत-पाक पर अपनी जान देनेवाले व्यक्तियों तथा बात-बात पर भूखा मरने वालों को याद किया तो वे एकदम सावधान हो गईं। उसने भक्तिन की संदेहयुक्त नज़र में छिपी हुई मनाही को तत्काल अनुभव कर लिया। भाव यह है कि उसे इस बात का पता लग गया कि उसका रसोई-घर में जाना निषेध है। अंततः भक्तिन द्वारा खींची गई कोयले की रेखा लेखिका के लिए लक्ष्मण-रेखा के समान सिद्ध हो गई, जिसे वह पार नहीं कर सकती थी अर्थात् भक्तिन ने अपनी पूजा-अर्चना के बाद लेखिका की रसोई पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
विशेष-
- यहाँ लेखिका ने भक्तिन द्वारा रसोई-घर में प्रवेश करने की प्रक्रिया पर समुचित प्रकाश डाला है।
- भक्तिन रसोई को लेकर छूत को मानती थी और चूल्हे-चौके की पवित्रता पर पूरा ध्यान देती थी।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वर्णनात्मक शैली द्वारा लेखिका ने भक्तिन के सुदृढ़ चरित्र पर प्रकाश डाला है।
- वाक्य-विन्यास बड़ा ही सटीक एवं सार्थक है।

गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) रसोई-घर में प्रवेश करने से पहले भक्तिन कौन-सा काम करती थी?
(ख) भक्तिन से निपटना लेखिका को टेढ़ी खीर क्यों लगा?
(ग) भक्तिन रसोई-घर में कोयले की मोटी रेखा क्यों खींचती थी?
(घ) किन कारणों से लेखिका भक्तिन की छुआछूत की प्रवृत्ति को सहन कर गई?
उत्तर:
(क) प्रतिदिन रसोई-घर में प्रवेश करने से पहले भक्तिन स्नान करती थी। तत्पश्चात् वह जल के छींटे मारकर अपने कपड़ों को पवित्र करती थी। सूर्य और पीपल को जल चढ़ाने के बाद वह दो मिनट तक नाक दबाकर जाप करती थी उसके बाद वह रसोई-घर में प्रवेश करती थी।
(ख) लेखिका को तत्काल पता चल गया कि भक्तिन एक दृढ़-निश्चय नारी है। उसे रसोई-घर की पवित्रता का पूरा ध्यान था। इस प्रकार के लोग अकसर पक्के इरादों वाले होते हैं। भक्तिन के द्वारा रसोई-घर में खींची गई कोयले की रेखा से लेखिका जान गई कि इससे निपटना टेढ़ी खीर है।
(ग) भक्तिन रसोई-घर में कोयले की रेखा खींच कर यह निश्चित करती थी कि रसोई बनाते समय कोई अन्य व्यक्ति रसोई-घर में घुसकर हस्तक्षेप न करे और न ही रसोई की पवित्रता को नष्ट करे।
(घ) लेखिका उन लोगों को याद करके भक्तिन की छुआछूत की प्रवृत्ति को सहन कर गई जो रसोई पकाने के मामले में ज़रा-सी भी चूक होने पर खाना-पीना छोड़ देते हैं अथवा अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
[8] भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती; पर ‘नरो वा कुंजरो वा’ कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर-उधर पड़े पैसे-रुपये, भंडार-घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर, उस संबंध में किसी . के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क-शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा-रुपया जो इधर-उधर पड़ा देखा, सँभालकर रख लिया। यह क्या चोरी है! उसके जीवन का परम कर्त्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है-जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है, उसे बदलकर इधर-उधर करके बताना, क्या झूठ है! इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते! [पृष्ठ-76]
प्रसंग – प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ में संकलित है। इसमें लेखिका भक्तिन के स्वभाव के गुणों तथा अवगुणों का मूल्यांकन करती हुई उसके चरित्र पर समुचित प्रकाश डालती है। लेखिका कहती है कि
व्याख्या – यह निर्णय करना बड़ा कठिन है कि भक्तिन एक अच्छी नारी है। कारण यह है कि उसमें कई दुर्गुण भी हैं। उसकी तुलना सत्यवादी हरिश्चंद्र से नहीं की जा सकती। लेकिन वह इस बात में विश्वास नहीं करती थी कि कोई बात सत्य है या असत्य। इसके लिए लेखिका ने युधिष्ठिर द्वारा कहे गए वाक्य ‘नरो वा कुंजरो वा’ का उदाहरण दिया है। भक्तिन लेखिका के घर में इधर-उधर पड़े रुपये-पैसे को उठाकर भंडार घर की किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी। वे पैसे-रुपये कहाँ पड़े हैं, इसका पता केवल भक्तिन को होता था।
इस संबंध में लेखिका यदि कोई आपत्ति करती तो वह शास्त्रार्थ करने लग जाती थी तथा बड़े से बड़ा तर्कशील व्यक्ति भी उसके तर्कों को सहन नहीं कर सकता था। फिर भी उसका यह कहना तर्क संगत था कि यह उसका अपना घर है। यदि उसने बिखरे पड़े पैसे-रुपये को संभालकर अपने पास रख लिया है तो यह कोई चोरी नहीं है, बल्कि यह तो उसका कर्तव्य है। उसके जीवन का सर्वोच्च कर्त्तव्य तो लेखिका को हमेशा प्रसन्न करना है।
उसका कहना था कि जिस बात पर लेखिका सकता है, उसे इधर-उधर बदलकर तथा थोडा-बहत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तत करना कोई झठ नहीं है, बल्कि ऐसा करके वह लेखिका के क्रोध को दूर करती है। उसका तर्क यह था कि धर्मराज महाराज भी इतनी चोरी तो करते ही होंगे और इतना झूठ तो बोलते ही होंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे भगवान को कैसे खुश कर पाते और संसार को कैसे चला पाते। भाव यह है कि भक्तिन हमेशा सच्चे-झूठे तर्क देकर इसमें सत्य सिद्ध करने में लगी रहती थी।
विशेष-
- यहाँ लेखिका ने भक्तिन के गुण-अवगुणों का सही मूल्यांकन किया है और उसकी तर्क देने की शक्ति पर प्रकाश डाला है।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वर्णनात्मक शैली द्वारा भक्तिन के चरित्र पर समुचित प्रकाश डाला गया है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा विषयानुकूल एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) लेखिका ने भक्तिन को अच्छा क्यों नहीं कहा?
(ख) सच-झूठ के बारे में भक्तिन का मूल दृष्टिकोण क्या था?
(ग) भक्तिन घर में इधर-उधर पडे रुपये-पैसे को भंडार-घर की मटकी में क्यों डाल देती थी?
(घ) भक्तिन का मूल लक्ष्य क्या था और वह उसे कैसे पूरा करती थी?
(ङ) भक्तिन रुपये-पैसे को मटकी में डालने को चोरी क्यों नहीं कहती थी?
उत्तर:
(क) भक्तिन के स्वभाव में गुणों के साथ-साथ कुछ अवगुण भी थे। सत्य-असत्य के बारे में उसकी अपनी राय थी। वह लोक-व्यवहार की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। इसलिए लेखिका ने भक्तिन को अच्छा नहीं कहा।
(ख) सच-झूठ के बारे में भक्तिन आचरण करने वाले व्यक्ति की नीयत को अधिक महत्त्व देती थी। वह महादेवी के घर में इधर-उधर पड़े रुपये-पैसे को मटकी में सँभालकर रख देती थी। उसका कहना था कि रुपये-पैसे को सँभालकर रखना कोई चोरी नहीं है।
(ग) भक्तिन घर में पड़े रुपये-पैसे को सँभालकर रखने के उद्देश्य से भंडार-घर की मटकी में डाल देती थी।
(घ) भक्तिन का मूल लक्ष्य अपनी मालकिन को प्रसन्न रखना था। इसके लिए वह सच-झूठ का सहारा लेने के लिए भी तैयार रहती थी। यदि उसकी किसी बात पर मालकिन क्रोधित हो जाती थी तो वह उस बात को रफा-दफा कर देती थी।
(ङ) भक्तिन पैसों को मटकी में डालने को चोरी इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि महादेवी के घर को सँभालना उसका काम था। इसलिए वह पैसे-रुपये को भी सँभालकर रखती थी। ऐसा करना वह चोरी नहीं समझती थी।
[9] पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है इसी से वह द्वार पर बैठकर बार-बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर:पुस्तकों को बाँधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आँचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुँचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है, इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक।। [पृष्ठ-78]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि भक्तिन महादेवी की एक अनन्य सेविका थी। जब महादेवी चित्रकला और कविता लिखने में व्यस्त होती थी, तो वह सहायता करने में असमर्थ होते हुए भी अपनी निष्ठा से कोई-न-कोई काम अवश्य ढूँढ़ लेती थी।
व्याख्या-जब महादेवी चित्रकला और काव्य-रचना में व्यस्त हो जाती थी, तो उस समय भक्तिन लेखिका का किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकती थी। परंतु इस स्थिति को स्वीकार करना भक्तिन को अपनी हीनता स्वीकार करना था। इसलिए वह द्वार पर बैठ जाती थी। वह बार-बार लेखिका से कोई-न-कोई काम बताने के लिए हठ करती रहती थी। कभी वह उत्तर:पुस्तिकाओं को बाँधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर और कभी चटाई को अपने आँचल से साफ कर लेखिका का सहयोग करती थी। लेखिका की बातों से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वह सामान्य व्यक्तियों से अधिक समझदार थी।
वह इस बात को अच्छी प्रकार से समझती थी कि जब अन्य लोग लेखिका का सहयोग करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, तब वह सक्रिय होकर अपने सहयोग की इच्छा को क्रियान्वित करती थी। यही कारण है कि जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होकर आती थी, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की किरणें प्रकाशमान हो उठती थीं। यह लगभग ऐसी ही स्थिति थी जैसे कि बिजली का बटन दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। भाव यह है कि जब भी महादेवी की कोई रचना पूर्ण होकर छपकर सामने आती थी, तो भक्तिन अत्यधिक प्रसन्न हो जाती थी। शायद वह यह सोचती थी कि महादेवी के लेखन में उसका भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा है।
विशेष-
- यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भक्तिन एक सच्ची सेविका के समान हमेशा उसका सहयोग करने के लिए तत्पर रहती थी।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास भावाभिव्यक्ति में सहायक है तथा ‘हाथ बँटाना’ मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है।
- वर्णनात्मक शैली द्वारा भक्तिन के चरित्र पर समूचा प्रकाश डाला गया है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) भक्तिन किस बात में स्वयं को हीन मानती है?
(ख) लेखिका की दृष्टि में भक्तिन अन्य सेवकों से अधिक बुद्धिमान कैसे है?
(ग) भक्तिन चित्रकला और कविता लिखने में लेखिका की किस प्रकार सहायता करती थी?
(घ) महादेवी की किसी पुस्तक के प्रकाशन पर भक्तिन कैसा अनुभव करती थी?
उत्तर:
(क) भक्तिन कभी खाली नहीं बैठ सकती थी। जब महादेवी चित्रकला और कविता लिखने में व्यस्त हो जाती थी, तो वह लेखिका की किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती थी। यही सोचकर वह स्वयं को हीन समझने लगी थी।
(ख) महादेवी द्वारा चित्रकला और कविता लिखने के दौरान अन्य सेवक स्वयं को असमर्थ समझते थे, परंतु भक्तिन तो महादेवी की सच्ची सेविका थी। वह अपनी निष्ठा से कोई-न-कोई काम अवश्य ढूँढ लेती थी। इसलिए वह अन्य सेवकों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमती थी।
(ग) भक्तिन चित्रकला और कविता लेखन के दौरान हमेशा महादेवी के पास ही बैठी रहती थी। वह हर प्रकार से महादेवी की सहायता करना चाहती थी। कभी तो वह अधूरे चित्र को कमरे के किसी कोने में रख देती थी, कभी चटाई को अपने आँचल से पोंछ देती थी। यही नहीं, वह दही का शरबत अथवा तुलसी की चाय देकर महादेवी की भूख को दूर करने का प्रयास करती रहती थी।
(घ) जब महादेवी की कोई रचना प्रकाशित होती थी, तो भक्तिन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता था। वह बार-बार पुस्तक को छूती थी और आँखों के निकट लाकर उसे देखती थी। वह यह सोचकर प्रसन्न होती थी कि इस पुस्तक के प्रकाशन में उसका भी थोड़ा-बहुत सहयोग है।
[10] मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बदरी-केदार आदि के ऊँचे-नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हठ करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गाँव की धूलभरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय, कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी-दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे; पर बहुत समझाने-बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है; रुपया भेज देती है; पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है; जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। [पृष्ठ-78-79]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2′ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ में संकलित है। यहाँ लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि भ्रमणकाल के दौरान भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ रहती थी। दूसरा, जब देश पर युद्ध के बादल मडराने लगे, तब उसकी बेटी और दामाद उसे लेने के लिए आए परंतु भक्तिन ने महादेवी के साथ रहना ही स्वीकार किया।
व्याख्या-लेखिका स्वीकार करती है कि भ्रमणकाल के दौरान भक्तिन हमेशा उसके साथ ही भ्रमण पर जाती थी। जब बदरी-केदार के ऊँचे-नीचे तथा तंग पहाड़ी रास्ते आ जाते तो वह हठपूर्वक महादेवी के आगे-आगे चल पड़ती, ताकि लेखिका को बिना किसी बाधा के चलने का मौका मिले। गाँव की धूल भरी पगडंडी में भक्तिन महादेवी के पीछे-पीछे चलना स्वीकार करती, ताकि महादेवी को गाँव की धूल परेशान न करे। जब भी महादेवी किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए तैयार होती तो भक्तिन छाया के समान उनके साथ चलती। भाव यह है कि भक्तिन हमेशा महादेवी की सेविका बनकर उनके साथ ही लगी रहती थी।
एक समय देश पर युद्ध के बादल मँडराने लगे थे, जिससे देश के सभी लोग भयभीत हो उठे थे। इस अवसर पर भक्तिन की बेटी और दामाद उसके नातियों को साथ लेकर भक्तिन को बुलाने के लिए महादेवी के घर आए। वे चाहते थे कि इस कष्ट के समय भक्तिन उनके साथ रहे, क्योंकि नगर युद्ध से अधिक प्रभावित होते हैं। इस अवसर पर भक्तिन को अनेक तर्क देकर समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु उसने किसी की बात नहीं सुनी और वह उनके साथ नहीं गई। वह समय-समय पर अपनी बेटी और उनके बच्चों को देख आती थी। यही नहीं, वह उनके पास रुपए भी भेज देती थी। यदि वह उनके साथ गाँव में जाकर रहती तो उसे लेखिका का साथ छोड़ना पड़ता। भक्तिन को यह कदापि स्वीकार नहीं था। वह तो जीवन के अंत तक महादेवी के साथ ही रहना चाहती थी।
विशेष-
- इसमें लेखिका ने भक्तिन की सच्ची सेवा-भक्ति पर प्रकाश डाला है जो हमेशा अपने सेवा-धर्म को निभाने के लिए छाया के समान उनके साथ लगी रहती थी।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है।
- वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है तथा ‘छाया के समान साथ रहना’ मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) तंग पहाड़ी रास्तों पर भक्तिन महादेवी के आगे-आगे क्यों चलती थी?
(ख) गाँव की धूलभरी पगडंडी पर भक्तिन महादेवी के पीछे-पीछे क्यों चलती थी?
(ग) युद्ध के दिनों में भक्तिन ने अपने गाँव जाना स्वीकार क्यों नहीं किया?
(घ) सिद्ध कीजिए कि भक्तिन महादेवी की एक सच्ची सेविका थी।
उत्तर:
(क) तंग पहाड़ी रास्तों में भक्तिन महादेवी के आगे-आगे इसलिए चलती थी, ताकि कोई खतरा न हो अथवा फिसलन या गड्ढा हो तो वह स्वयं उसका सामना करे। महादेवी को किसी खतरे का सामना न करना पड़े।
(ख) गाँव की धूलभरी पगडंडी पर भक्तिन महादेवी के पीछे-पीछे इसलिए चलती थी, ताकि महादेवी को रास्ते की धूल परेशान न करे अथवा वह स्वयं उस धूल को अपने ऊपर झेल लेती थी।
(ग) युद्ध के दिनों में नगर के लोगों पर खतरा मँडराने लगा था। नगर के सभी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। इसीलिए भक्तिन की बेटी और दामाद उसे गाँव में ले जाने के लिए आए थे। परंतु भक्तिन ने महादेवी को अकेला छोड़कर उनके साथ गाँव जाना स्वीकार नहीं किया और प्रत्येक स्थिति में महादेवी के साथ रहना पसंद किया।
(घ) निश्चय से भक्तिन महादेवी की एक सच्ची सेविका थी। वह अपने सेवा-धर्म में प्रवीण थी और छाया के समान अपनी स्वामिन के साथ रहती थी। तंग रास्तों पर वह महादेवी के आगे चलती थी, ताकि वह पहले खतरे का सामना कर सके। गाँव की धूलभरी पगडंडी पर वह महादेवी के पीछे चलती थी, ताकि महादेवी को गाँव की धूल-मिट्टी का सामना न करना पड़े। युद्ध के दिनों में भी उसने महादेवी के साथ रहना ही पसंद किया।

[11] भक्तिन और मेरे बीच में सेवक-स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया, जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हँस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, जितना अपने घर में बारी-बारी से आने-जाने वाले अँधेरे-उजाले और आँगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख-दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। [पृष्ठ-79]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि उसने भक्तिन को अपनी सेविका न मानकर अपनी सहयोगी स्वीकार किया है। लेखिका लिखती है कि
व्याख्या-यह कहना लगभग असंभव है कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध रहा होगा। संसार में ऐसा कोई स्वामी नहीं है, जो चाहने पर भी अपने सेवक को सेवा-कार्य से हटा न सके अर्थात् चाहने पर भी महादेवी भक्तिन को सेवा-कार्य से मुक्त नहीं कर सकी। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई सेवक भी नहीं हो सकता, जिसे स्वामी ने यह आदेश दिया हो कि वह काम छोड़कर चला जाए और वह स्वामी के आदेश को न मानता हुआ केवल हँस पड़े। जब भी महादेवी भक्तिन को काम छोड़कर जाने की आज्ञा देती थी, तो वह आगे से हँस देती थी, काम छोड़कर जाना तो एक अलग बात है।
महादेवी की दृष्टि में भक्तिन को घर का नौकर कहना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार घर में बारी-बारी अंधेरा और उजाला आता रहता है, गुलाब खिलता रहता है और आम फलता रहता है, परंतु हम उन्हें नौकर नहीं कह सकते, यह उनका स्वभाव है। इन सबका अपना-अपना अस्तित्व है, जिसे सार्थक बनाने के लिए वह हमें सुख और दुख देते रहते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का अस्तित्व भी स्वतंत्र था और वह अपने विकास का परिचय देने के लिए लेखिका को चारों ओर से घेरे हुए थी। भाव यह है कि भक्तिन महादेवी के जीवन का एक अनिवार्य अंग थी, अपने सुख-दुख दोनों के साथ जीवित रहने की अधिकारिणी थी।
विशेष-
- इसमें लेखिका ने भक्तिन और अपने जीवन के प्रगाढ़ संबंधों पर समुचित प्रकाश डाला है।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित तथा भावानुकूल है।
- वर्णनात्मक शैली द्वारा भक्तिन के जीवन-चरित्र पर समुचित प्रकाश डाला गया है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) महादेवी भक्तिन को अपनी सेविका क्यों नहीं मानती थी?
(ख) जब महादेवी ने भक्तिन को वहाँ से चले जाने का आदेश दिया तो भक्तिन ने कैसा व्यवहार किया?
(ग) भक्तिन और महादेवी के बीच किस प्रकार का संबंध था?
(घ) लेखिका ने अंधेरे, उजाले, गुलाब, आम द्वारा भक्तिन में क्या समानता खोजी है?
उत्तर:
(क) महादेवी भक्तिन को अपनी सेविका नहीं मानती थी, क्योंकि वह चाहकर भी उसको नौकरी से नहीं हटा सकती थी और यदि वह उसको ऐसा कहती तो भक्तिन हँसी में ही उसकी बात को टाल जाती थी। वह उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पाती थी। इसलिए महादेवी उसको सेविका नहीं मानती थी।
(ख) जब महादेवी ने भक्तिन को नौकरी छोड़कर चले जाने का आदेश दिया तो उसने महादेवी के आदेश की अवज्ञा की और हँस दिया। वह तो स्वयं को महादेवी की संरक्षिका मानती थी। इसलिए वह उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी।
(ग) भक्तिन और महादेवी के बीच प्रगाढ़ आत्मीयता थी। वस्तुतः भक्तिन स्वयं को महादेवी की संरक्षिका मानती थी, इसलिए वह उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उसके और भक्तिन के बीच सेविका और स्वामिन का संबंध नहीं था।
(घ) लेखिका का कहना है कि जिस प्रकार घर में अँधेरे, उजाले, गुलाब तथा आम का अलग-अलग अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से भक्तिन का भी घर में अलग स्थान था। वह लेखिका की केवल सेविका नहीं थी, बल्कि सुख-दुख में साथ देने वाली अनन्य सहयोगी भी थी।
[12] मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है; पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा, मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सदभाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहजबुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार-प्रकार और वेश-भूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है; पर आदर-भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त-व्यस्त वेश-भूषा देखकर वह कह उठती है- ‘का ओहू कवित्त लिखे जानत हैं और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है- तब ऊ कुच्छौ करिहैं-धरि, ना-बस गली-गली गाउत-बजाउत फिरिहैं। [पृष्ठ-80]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संर अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। भक्तिन महादेवी के साहित्यिक बंधुओं पर पूरी नज़र रखती थी और यह जानने का प्रयास करती थी कि उनमें से कौन महादेवी का आदर-सम्मान करते थे।
व्याख्या-महादेवी लिखती है कि भक्तिन उसके साहित्यिक बंधुओं को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन वह उन्हीं साहित्यिक बंधुओं को सम्मान देती थी, जो महादेवी का उचित सम्मान करते थे। उनके प्रति भक्तिन की सद्भावना इस बात पर निर्भर करती थी कि वे लेखिका के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं। भक्तिन की इस प्रकार की सहज बुद्धि देखकर लेखिका स्वयं आश्चर्यचकित हो जाती। वह किसी साहित्यिक बंध के आकार-प्रकार और कपड़ों से उनको याद करती थी और किसी को उसके बिगड़े नाम से याद करती थी।
कवि और कविता के बारे में उसका ज्ञान बढ़ चुका था। परंतु वह हरेक का आदर-सम्मान नहीं करती थी। किसी कवि के लंबे-लंबे बाल तथा अस्त-व्यस्त कपड़े देखकर यह कह उठती थी कि क्या यह भी कविता लिखना जानता है। इसके साथ ही वह अपनी अवज्ञा को स्पष्ट करते हुए कहती थी कि क्या यह कुछ काम-धाम करता है या गली-गली में गाता बजाता फिरता है। भाव यह है कि लंबे-लंबे बालों वाले तथा अस्त-व्यस्त कपड़ों वालों को वह पसंद नहीं करती थीं।
विशेष-
- यहाँ लेखिका ने भक्तिन की सहज बुद्धि पर प्रकाश डाला है जो साहित्यिक बंधुओं द्वारा अपनी स्वामिनी के प्रति किए गए सम्मान को देखकर ही उनका मूल्यांकन करती है।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा सटीक एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है।
- संवादात्मक तथा वर्णनात्मक शैलियों के द्वारा भक्तिन के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) भक्तिन महादेवी के साहित्यिक बंधुओं का आदर-सम्मान किस प्रकार करती है?
(ख) भक्तिन साहित्यिक बंधुओं को किस नाम से याद करती है?
(ग) किन लोगों के प्रति भक्तिन अपनी अवज्ञा प्रकट करती है?
(घ) किस प्रकार के साहित्यिक मित्रों के प्रति भक्तिन सद्भाव रखती है?
उत्तर:
(क) भक्तिन महादेवी वर्मा के साहित्यिक बंधुओं का आदर-सम्मान इस आधार पर करती है कि वे लोग महादेवी का कितना सम्मान करते हैं। यदि कोई साहित्यकार महादेवी का अत्यधिक आदर-सम्मान करता है तो वह भी उसका अत्यधिक आदर-सम्मान करती है अन्यथा नहीं।
(ख) भक्तिन साहित्यिक बंधुओं को उनकी वेश-भूषा, रूप, आकार अथवा उनके नाम के बिगड़े हुए रूप से याद करती है।
(ग) जो साहित्यिक बंधु लंबे-लंबे बालों तथा अस्त-व्यस्त कपड़ों के साथ आते थे, उन्हें भक्तिन बेकार आदमी समझती थी। ऐसे व्यक्तियों के प्रति भक्तिन अपनी अवज्ञा प्रकट करती है।
(घ) जो साहित्यिक मित्र महादेवी के प्रति सद्भाव रखते थे, उन्हीं के प्रति भक्तिन भी सद्भाव रखती थी।
[13] भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है, जैसे यमलोक से। ऊँची दीवार देखते ही, वह आँख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमज़ोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता-बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा; पर डर से भी अधिक महत्त्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या-क्या सामान बाँध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती, जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। [पृष्ठ-80]
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक ‘आरोह भाग 2’ में संकलित पाठ ‘भक्तिन’ नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र से अवतरित है। यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की महान कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के चरित्र की एक अन्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। भले ही भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी, लेकिन वह अपनी स्वामिनी के जेल जाने पर उनके साथ जेल जाने को तैयार हो जाती है।
व्याख्या-भक्तिन के मन में कुछ ऐसे संस्कार पड़ गए थे कि वह जेल को यमलोक मानकर अत्यधिक भयभीत हो जाती थी। ऊँची दीवार को देखते ही वह अपनी आँखें बंदकर बेहोश हो जाना चाहती थी। उसकी इस कमज़ोरी का सबको पता लग गया था। इसलिए प्रायः लोग उसे यह कहकर चिढ़ाते और डराते थे कि महादेवी को जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। यह कहना तो झूठ होगा कि वह डरती नहीं थी। परंतु उसके लिए साथ रहने का महत्त्व डर से भी अधिक था। कभी-कभी वह चुपचाप लेखिका से पूछ लेती कि वह अपनी कितनी धोतियों को साफ कर ले, ताकि वहाँ जाने पर उसे शर्मिन्दा न होना पड़े।
कभी-कभी वह यह भी पूछ लेती कि जेल जाने के लिए उसे कौन-सा सामान बाँधकर तैयार कर लेना चाहिए, जिससे लेखिका को जेल जाने में कोई तकलीफ न हो। जेल-यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, बल्कि उसे अकेले ही जेल जाना होता है, परंतु यह बात भक्तिन के लिए कोई महत्त्व नहीं रखती थी। महादेवी के जेल जाने की कल्पना से भक्तिन इतनी अधिक दुखी नहीं थी, जितनी कि इस बात को लेकर कि वह अपनी मालकिन के साथ जेल नहीं जा सकती। इस अपमान की संभावना से ही वह डर जाती थी, क्योंकि वह तो हमेशा अपनी मालकिन के साथ रहना चाहती थी। कहने का भाव यह है कि भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने को भी तैयार थी।
विशेष-
- इसमें लेखिका ने भक्तिन की एकनिष्ठ सेवा-भावना का संवेदनशील वर्णन किया है।
- सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है।
- वाक्य-विन्यास सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक है।
- वर्णनात्मक और संवादात्मक शैलियों के प्रयोग द्वारा भक्तिन के चरित्र पर समुचित प्रकाश डाला गया है।
गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(क) भक्तिन कारागार से क्यों डरती थी?
(ख) डरते हुए भी भक्तिन कारागार जाने की तैयारी क्यों करने लगती है?
(ग) महादेवी को किन कारणों से कारागार जाना पड़ सकता था?
(घ) सिद्ध कीजिए भक्तिन एक सच्ची स्वामी-सेविका है?
उत्तर:
(क) भक्तिन ने बाल्यावस्था से ही जेल के बारे में बड़ी भयानक बातें सुन रखी थीं। इसलिए वह जेल के नाम से ही डरती थी। दूसरे शब्दों में, वह अपने संस्कारों के कारण भी जेल जाने से डरती थी।
(ख) भले ही भक्तिन जेल से बहुत डरती थी, परंतु अपनी मालकिन से अलग रहना उसके लिए अधिक कष्टकर था। इसलिए वह किसी भी स्थिति में लेखिका का साथ नहीं छोड़ सकती थी। अतः वह जेल जाने की तैयारी करने लगती है।
(ग) स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में लेखिका को कारागार जाना पड़ सकता था, क्योंकि उन दिनों देश में स्वतंत्रता आंदोलन ज़ोर-शोर से चल रहा था।
(घ) भक्तिन सही अर्थों में अपनी मालकिन की सच्ची सेविका है। वह निजी सुख-दुख अथवा कारागार के भय की परवाह न करके अपनी मालकिन की सेवा करना चाहती है। वह छाया के समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती है। जब उसे यह बताया जाता था कि महादेवी को जेल जाना पड़ सकता है तो वह भी जेल जाने को तैयार हो जाती थी।
भक्तिन Summary in Hindi
भक्तिन लेखिका-परिचय
प्रश्न-
महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
1. जीवन-परिचय-महादेवी वर्मा का जन्म सन् 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल, इंदौर में हुई। नौ वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें विवाह के बंधन में बाँध दिया गया था, किंतु यह बंधन स्थाई न रह सका। उन्होंने अपना सारा समय अध्ययन में लगाना प्रारंभ कर दिया और सन् 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें छायावादी हिंदी काव्य के चार स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्हें विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सन् 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण अलंकरण से सम्मानित किया। उन्हें 1983 में ‘यामा’ संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती-पुरस्कार मिला। उन्हें विक्रम विश्वविद्यालय, कुमायूँ विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट् की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। 11 दिसंबर, 1987 को उनका देहांत हो गया।
2. प्रमुख रचनाएँ महादेवी वर्मा ने कविता, रेखाचित्र, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना की हैं। उन्होंने ‘चाँद’ और ‘आधुनिक कवि काव्यमाला’ का संपादन कार्य भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं
काव्य-संग्रह ‘नीहार’, ‘रश्मि’, ‘नीरजा’, ‘सांध्यगीत’, ‘दीपशिखा’, ‘यामा’ आदि।
निबंध-संग्रह- शृंखला की कड़ियाँ’, ‘क्षणदा’, ‘संकल्पिता’, ‘भारतीय संस्कृति के स्वर’, ‘आपदा’।
संस्मरण/रेखाचित्र-संग्रह ‘अतीत के चलचित्र’, ‘स्मृति की रेखाएँ’, ‘पथ के साथी’, ‘मेरा परिवार’।
आलोचना-‘हिंदी का विवेचनात्मक गद्य’, ‘विभिन्न काव्य-संग्रहों की भूमिकाएँ।

3. साहित्यिक विशेषताएँ महादेवी वर्मा कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन गद्य के विकास में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध आदि गद्य विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उनके अधिकांश संस्मरण एवं रेखाचित्र कहानी-कला के समीप दिखाई पड़ते हैं। उनके संस्मरणों के पात्र अत्यंत सजीव एवं यथार्थ के धरातल पर विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। उनकी गद्य रचनाओं में अनुभूति की प्रबलता के कारण पद्य जैसा आनंद आता है। उनके संस्मरणों के मानवेत्तर पात्र भी बड़े सहज एवं सजीव बन पड़े हैं। उनके गद्य साहित्य की मूल संवेदना करुणा और प्रेम है। इसीलिए उनका गद्य साहित्य काव्य से भिन्न है। काव्य में वे प्रायः अपने ही सुख-दुख, विरह-वियोग आदि की बातें करती रही हैं, किंतु उन्होंने गद्य साहित्य में समाज के सुख-दुख का अत्यंत मनोयोग से चित्रण किया है। उनके द्वारा लिखे गए रेखाचित्रों में समाज के दलित वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों के बड़े मार्मिक चित्र मिलते हैं। इनमें उन्होंने उच्च समाज द्वारा उपेक्षित, निम्न कहे जाने वाले उन लोगों का चित्रण किया है, जिनमें उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अधिक मानवीय गुण और शक्ति है। अतः स्पष्ट है कि उनका गद्य साहित्य समाजपरक है।
उनके गद्य साहित्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं और परिस्थितियों का भी यथार्थ चित्रण हुआ है। नारी समस्याओं को भी उन्होंने अपनी कई रचनाओं के माध्यम से उठाया है। वे काव्य की भाँति गद्य की भी महान साधिका रही हैं। उनके गद्य साहित्य में उनका कवयित्री-रूप भी लक्षित होता है।
4. भाषा-शैली-महादेवी जी के गद्य की भाषा-शैली अत्यंत सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। उनकी गद्य भाषा में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। महादेवी की गद्य-शैली वैसे तो उनकी काव्य-शैली के ही समान संस्कृतगर्भित, भाव-प्रवण, मधुर और सरस है, परंतु उसमें अस्पष्टता और दुरूहता नहीं है। इसे व्यावहारिक शैली माना जा सकता है। कहीं-कहीं विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु बहुत ही कम। उनकी रचनाओं की भाषा-शैली की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मर्मस्पर्शिता है। वे भावुक होकर पात्रों की दीन-हीन दशा, उनके मानसिक भावों तथा वातावरण का बड़ा मार्मिक चित्रण करती हैं। उनका काव्य व्यंग्य और हास्य से शून्य है, परंतु वे अपनी गद्य-रचनाओं में समाज, धर्म, व्यक्ति और विशेष रूप से पुरुष जाति पर बड़े गहरे व्यंग्य कसती हैं। बीच-बीच में हास्य के छींटे भी उड़ाती चलती हैं। इन विशेषताओं ने उनके गद्य को बहुत आकर्षक, मधुर और प्रभावशाली बना दिया है। वे प्रायः व्यंजना-शक्ति से काम लेती हैं। वे अपनी इस आकर्षक गद्य-शैली द्वारा हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव डालती हैं। संक्षेप में, उनकी गद्य-शैली में कल्पना, भावुकता, सजीवता और भाषा-चमत्कार आदि के एक-साथ दर्शन होते हैं। उसमें सुकुमारता, तरलता और साथ ही हृदय को उद्वेलित कर देने की अद्भुत शक्ति भी है।
भक्तिन पाठ का सार
प्रश्न-
महादेवी वर्मा द्वारा रचित ‘भक्तिन’ नामक संस्मरण का सार अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
भक्तिन’ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। यह उनकी प्रसिद्ध रचना ‘स्मृति की रेखाएँ’ में संकलित है। भक्तिन महादेवी वर्मा की एक समर्पित सेविका थी। उन्होंने इस रेखाचित्र में अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। प्रस्तुत पाठ का सार इस प्रकार है
1. भक्तिन का व्यक्तिगत परिचय-भक्तिन छोटे कद की तथा दुबले शरीर की नारी थी। उसके होंठ बहुत पतले और आँखें छोटी थीं, जिनसे उनका दृढ़ संकल्प और विचित्र समझदारी झलकती थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। अहीर कुल में जन्मी इस नारी की आयु 75 साल के लगभग थी। उसका नाम लक्ष्मी (लछमिन) था, लेकिन उसने लेखिका से यह निवेदन किया कि उसे नाम से न पुकारा जाए। उसके गले में कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसे ‘भक्तिन’ कहना शुरू कर दिया। अहीर कुल में जन्मी भक्तिन सेवा धर्म में अत्यधिक निपुण थी। लेखिका ने भक्तिन की कर्मठता, उनके प्रति लगाव व सेविका धर्म के कारण उसकी तुलना अंजनी-पुत्र महावीर हनुमान जी से की है। वह विनम्र स्वभाव की नारी थी।
2. भक्तिन के गृहस्थी जीवन का आरंभ-भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक गाँव झूसी में हुआ था। वह एक अहीर की इकलौती बेटी थी तथा उसकी विमाता ने ही उसका लालन-पालन किया था। पाँच वर्ष की अल्पायु में लक्ष्मी का विवाह हँडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया और नौ वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया। इधर भक्तिन के पिता का देहांत हो गया। लेकिन विमाता ने देर से मृत्यु का समाचार भेजा। सास ने रोने-धोने के अपशकुन के डर से लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद सास ने लक्ष्मी को अपने मायके जाकर अपने माता-पिता से मिल आने को कहा। घर पहुँचते ही विमाता ने उसके साथ बड़ा कटु व्यवहार किया। अतः लक्ष्मी वहाँ से पानी पिए बिना ही अपने ससुराल चली आई। ससुराल में अपनी सास को खरी-खोटी सुनाकर अपनी विमाता पर आए हुए गुस्से को शांत किया और अपने पति पर अपने गहने फेंकते हुए अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। तब लक्ष्मी अपनी ससुराल में टिक कर रहने लगी।
भक्तिन को आरंभ से ही सुख नसीब नहीं हुआ। उसकी एक के बाद एक निरंतर तीन बेटियाँ उत्पन्न हुईं। फलतः सास तथा जिठानियाँ उसकी उपेक्षा करने लगीं। सास के तीन कमाने वाले.पुत्र थे और दोनों जिठानियों के भी पुत्र थे। धीरे-धीरे भक्तिन को घर के सारे काम-काज़ में लगा दिया गया। चक्की चलाना, कूटना-पीसना, खाना बनाना आदि सभी उसे करना पड़ता था। उसकी तीनों बेटियाँ गोबर उठाती और उपले पाथती थीं। खाने-पीने में भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था। जिठानियों तथा उनके बेटों को दूध मलाई युक्त पकवान मिलता था, परंतु भक्तिन तथा उसकी लड़कियों को काले गुड़ की डली और चने-बाजरे की घुघरी खाने को मिलती थी। यह सब होने पर भी भक्तिन खुश थी। क्योंकि उसका पति बड़ा मेहनती तथा सच्चे मन से उसे प्यार करता था। यही सोचकर भक्तिन अपने संयुक्त परिवार से अलग हो गई। परिवार से अलग होते ही उसको गाय-भैंस, खेत-खलिहान और अमराई के पेड़ मिल गए थे, पति-पत्नी दोनों ही मेहनती थे, अतः घर में खुशहाली आ गई।
3. भक्तिन के पति का देहांत-पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो बड़े धूमधाम से किया, परंतु अभी दोनों छोटी लड़कियाँ विवाह योग्य नहीं थीं। अचानक भक्तिन पर प्रकृति की गाज गिर गई। उसके पति का देहांत हो गया। उस समय भक्तिन की आयु उनतीस वर्ष थी। संपत्ति के लालच में परिवार के लोगों ने उसके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु वह सहमत नहीं हुई। उसने अपने सिर के बाल कटवा दिए और गुरुमंत्र लेकर गले में कंठी धारण कर ली। वह स्वयं अपने खेतों की देख-रेख करने लगी। दोनों छोटी बेटियों का विवाह करने के बाद उसने बड़े दामाद को घरजमाई बना लिया। परंतु बदकिस्मती तो भक्तिन के साथ लगी हुई थी। शीघ्र ही उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की नज़र अब भी भक्तिन की संपत्ति पर थी। भक्तिन के जेठ का बना लड़का विधवा बहन का विवाह अपने तीतरबाज़ साले से कराना चाहता था। परंतु भक्तिन की विधवा लड़की ने अस्वीकार कर दिया। अब माँ-बेटी दोनों ही अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी।
तीतरबाज बेटी की कोठरी में जा घुसा और उसने भीतर से द्वार बंद कर दिया। इसी बीच तीतरबाज़ के समर्थकों ने गाँव वालों को वहाँ बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने तीतरबाज़ की अच्छी प्रकार पिटाई की और कुंडी खोल दी और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन तीतरबाज़ ने यह तर्क दिया कि वह तो लड़की के बुलाने पर कमरे में दाखिल हुआ था। आखिर में गाँव में पंचायत बुलाई गई। भक्तिन की बेटी ने बार-बार तर्क दिया कि यह तीतरबाज़ झूठ बोल रहा है अन्यथा वह उसकी पिटाई क्यों करती। परंतु पंचों ने कलयुग को ही इस समस्या का मूल कारण माना और यह आदेश दे दिया कि वह अब दोनों पति-पत्नी के रूप में रहेंगे। भक्तिन और उसकी बेटी कुछ भी नहीं कर पाए। यह विवाह सफल नहीं हुआ। तीतरबाज़ एक आवारा किस्म का आदमी था और कोई काम-धाम नहीं करता था। अतः भक्तिन का घर गरीबी का शिकार बन गया। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि लगान चुकाना भी कठिन हो गया। जमींदार ने भक्तिन को भला-बुरा कहा और दिन-भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वह कमाई के विचार से दूसरे ही दिन शहर चली गई।

4. भक्तिन के जीवन के दुख का अंतिम पड़ाव-घुटी हुई चाँद, मैली धोती तथा गले में कंठी धारण करके भक्तिन जब पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए उपस्थित हुई तो उसने बताया कि वह दाल-भात राँधना, सब्जी छौंकना, रोटी बनाना आदि रसोई के सभी काम करना जानती है। लेखिका ने शीघ्र ही उसे काम पर रख लिया। अब भक्तिन एक पावन जीवन व्यतीत करने लगी। नौकरी पर लगते ही उसने सवेरे-सवेरे स्नान किया। लेखिका की धुली हुई धोती को उसने जल के छींटों से पवित्र किया और फिर पहना। तत्पश्चात् उसने सूर्योदय और पीपल को जल चढ़ाया। दो मिनट तक जाप करने के बाद चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना आरंभ किया। वह छूत-पाक को बहुत मानती थी। अतः लेखिका को भी समझौता करना पड़ा। वह नाई के उस्तरे को गंगाजल से धुलवाकर अपना मुंडन करवाती थी। अपना खाना वह अलग से ऊपर के आले में रख देती थी।
5. भक्तिन की नौकरी का श्रीगणेश-भक्तिन ने जो भोजन बनाया, वह ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का था। उसने कोई सब्जी नहीं बनाई, केवल दाल बनाकर मोटी-मोटी रोटियाँ सेंक दी जो कुछ-कुछ काली हो गई थीं। लेखिका ने जब इस भोजन को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, तब भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गाँव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। मजबूर होकर लेखिका ने दाल से एक रोटी खाई और विश्वविद्यालय चली गई। वस्तुतः लेखिका ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए ही भक्तिन को अपने घर पर भोजन बनाने के लिए रखा था। परंतु उस वृद्धा भक्तिन की सरलता के कारण वह अपनी असुविधाओं को भूल गई।
6. विचित्र स्वभाव की नारी-भक्तिन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह हमेशा दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती थी और स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। स्वयं लेखिका भी भक्तिन की तरह ग्रामीण बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों-की-त्यों ग्रामीण ही रही। शीघ्र ही उसने लेखिका को ग्रामीण खान-पान के अधीन बना दिया, किंतु स्वयं कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया और न ही ‘आँय’ कहने की आदत बदलकर ‘जी’ कह सकी। भक्तिन बड़ी व्यावहारिक महिला थी। वह अकसर लेखिका के बिखरे पड़े पैसों को. मटकी में छिपाकर रख देती थी। उसके लिए यह कोई बुरा काम नहीं था।
उसका कहना था कि घर में बिखरा हुआ पैसा-टका उसने सँभालकर रख दिया है। कई बार वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए किसी बात को पलट भी देती थी। उसके विचारानुसार यह झूठ नहीं था। एक बार लेखिका ने उसे सिर मुंडाने से रोकने का प्रयास किया। तब उसने यह तर्क दिया “तीरथ गए मुँडाए सिद्ध।” भक्तिन पूर्णतः अनपढ़ थी। उसे हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। लेखिका ने जब उसे पढ़ने-लिखने को कहा, तब उसने यह तर्क दिया कि मालकिन तो हर समय पढ़ती रहती है, अगर वह भी पढ़ने लग गई तो घर का काम कौन देखेगा।
7. स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठावान-भक्तिन को अपनी मालकिन पर बड़ा गर्व था। उसकी मालकिन जैसा काम कोई भी करना नहीं जानता था, उसके कहने पर भी उत्तर:पुस्तिकाओं के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया। परंतु भक्तिन ने मालकिन की सहायता की। वह कभी उत्तर:पुस्तिकाओं को बाँधती, कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में रखती, कभी रंग की प्याली धोकर साफ करती और कभी चटाई को अपने आँचल से झाड़ती थी। इसलिए वह समझती थी कि मालकिन दूसरों की अपेक्षा विशेष है। जब भी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। वह सोचती थी कि प्रकाशित रचना में उसका भी सहयोग है।
अनेक बार लेखिका भक्तिन के बार-बार कहने पर भी भोजन नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन को कभी दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा-भावना कूट-कूट कर स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन को कभी दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा-भावना कूट-कूट कर भरी थी। छात्रावास की रोशनी बुझ जाने के बाद लेखिका के परिवारिक सदस्य सोना हिरनी, बसंत कुत्ता, गोधूलि बिल्ली आदि आराम करने लग जाते थे। परंतु भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। वह आवश्यकता पड़ने पर मालकिन को पुस्तक पकड़ाती या स्याही लाकर देती या फाइल । यद्यपि भक्तिन देर रात को सोती थी, परंतु प्रातः मालकिन के जागने से पहले उठ जाती थी और वह सभी पशुओं को बाड़े से बाहर निकालती थी।
8. भक्तिन की मालकिन के प्रति भक्ति-भावना-भ्रमण के समय भी भक्तिन लेखिका के साथ रहती थी। बदरी-केदार के ऊँचे-नीचे तंग पहाड़ी रास्तों पर वह हमेशा अपनी मालकिन के आगे-आगे चलती थी। परंतु यदि गाँव की धूलभरी पगडंडी आ जाती तो वह लेखिका के पीछे चलने लगती। इस प्रकार वह हमेशा लेखिका के साथ अंग रक्षक के रूप में रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे तब भी वह अपनी बेटी और दामाद के बार-बार कहने पर लेखिका को नहीं छोड़ती थी।
जब उसे पता चला कि युद्ध में भारतीय सैनिक हार रहे हैं, तो उसने लेखिका को अपने गाँव चलने के लिए कहा और कहा कि उसे गाँव में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। भक्तिन स्वयं को लेखिका का अनिवार्य अंग मानती थी। उसका कहना था कि मालकिन और उसका संबं ध स्वामी-सेविका का संबंध नहीं है। वह कहती थी कि मालकिन उसे काम से हटा नहीं सकती। जब मालकिन उसे चले जाने की आज्ञा देती तो वह हँसकर टाल देती थी। इस प्रकार वह हमेशा छाया के समान लेखिका के साथ जुड़ी हुई थी। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहती थी।
9. छात्रावास की बालिकाओं की सेवा भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर पिलाती थी। कभी-कभी वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी चखाती थी। जो परिचित लेखिका का सम्मान करते थे, उन्हीं के साथ वह अच्छा व्यवहार करती थी। लेखिका के परिचितों को वह नाम से या आकार-प्रकार, वेशभूषा से जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में कोई आदर-भाव नहीं था। परंत दूसरों के दख से वह अत्यधिक दुखी हो जाती थी। जब कभी उसे किसी विद्यार्थी के जेल जाने की खबर मिली तो वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसे जेल से बहुत डर लगता था, किंतु लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार थी। उसका कहना था कि ऐसा करने के लिए उसे बड़े लाट से लड़ना पड़ा तो वह लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इस प्रकार लेखिका के साथ भक्तिन का प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। भक्तिन की कहानी को लेखिका ने अधूरा ही रखा है।
कठिन शब्दों के अर्थ
संकल्प = मज़बूत इरादा, पक्का निश्चय। जिज्ञासु = जानने का इच्छुक। चिंतन = सोच-विचार। मुद्रा = भाव-स्थिति। कंठ = गला। पचै = पचास । बरिस = वर्ष । संभवतः = शायद। स्पर्धा = मुकाबला। अंजना = हनुमान की माता। गोपालिका = अहीर की पत्नी अहीरन। दुर्वह = धारण करने में कठिन। समृद्धि = संपन्नता। कपाल = मस्तक। कुंचित = सिकुड़ी हुई। शेष इतिवृत्त = बाकी कथा। पूर्णतः = पूरी तरह से। अंशतः = थोड़ा-सा। विमाता = सौतेली माँ। किंवदंती = लोक प्रचलित कथन। ममता = स्नेह। वय = आयु। संपन्न = अमीर, धनवान। ख्याति = प्रसिद्धि। गौना = पति के घर दूसरी बार जाने की परिपाटी। अगाध = अत्यधिक गहरा। ईर्ष्यालु = ईर्ष्या करने वाली। सतर्क = सावधान। मरणांतक = मृत्यु देने वाला। नैहर = मायका। अप्रत्याशित = जिसकी आशा न हो। अनुग्रह = कृपा। अपशकुनी = बदशकुनी। पुनरावृत्तियाँ = बार-बार कही गई बातें। ठेल ले जाना = पहुँचाना। लेश = तनिक। शिष्टाचार = सभ्य व्यवहार। शिथिल = थकी हुई। विछोह = वियोग। मर्मव्यथा = हृदय को कष्ट देने वाली वेदना। विधात्री = जन्म देने वाली माँ। मचिया = छोटी चारपाई। पुरखिन = बड़ी-बूढ़ी। अभिषिक्त = विराजमान। काक-भुशंडी = कौआ।
सृष्टि = उत्पन्न करना। लीक = परंपरा। क्रमबद्ध = क्रमानुसार। विरक्त = विरागी। परिणति = परिणाम। धमाधम = ज़ोर-ज़ोर से। चुगली-चबाई = निंदा-बुराई। परिश्रमी = मेहनती। तेजस्विनी = तेजवान। अलगौझा = अलग होना। पुलकित = प्रसन्न। दंपति = पति-पत्नी। खलिहान = पकी हुई फसल को काटकर रखने का स्थान। कुकरी = कुतिया। बिलारी = बिल्ली। जिगतों = जेठ का पुत्र । घरौंदा = घर। बुढ़ऊ = बूढ़ा। होरहा = हरे अनाज का आग पर भूना रूप। अजिया ससुर = पति का बाबा। उपार्जित = कमाई। काकी = चाची। दुर्भाग्य = बदकिस्मती। भइयहू = छोटी भाभी। परास्त = हराना। गठबंधन = विवाह। निमंत्रण = बुलावा। परिमार्जन = शुद्ध करना। कर्मठता = कर्मशीलता। आहट = हल्की-सी आवाज । दीक्षित होना = स्वीकार करना। सम्मिश्रण = मिला-जुला रूप। अभिनंदन = स्वागत। उपरांत = बाद में। प्रतिष्ठित = स्थापित। टेढ़ी खीर = कठिन कार्य । वीतराग = विरक्त। पाक-विद्या = भोजन बनाने की विद्या। शंकाकुल दृष्टि = संदेह की नज़र। दुर्लध्य = पार न की जा सकने वाली। निरुपाय = उपायहीन। निर्दिष्ट = निश्चित। पितिया ससुर = पति के चाचा। आप्लावित = फैली हुई। आरोह (भाग 2) [भक्तिना सारगर्भित लेक्चर = संक्षिप्त भाषण। अरुचि = रुचि न रखना।
यूनिवर्सिटी = विश्वविद्यालय। चिंता-निवारण = चिंता दूर करना। उपचार = इलाज। असुविधाएँ = कठिनाइयाँ । प्रबंध = व्यवस्था। जाग्रत = सचेत । दुर्गुण = अवगुण। क्रियात्मक = क्रियाशील । दंतकथाएँ = परंपरा से चली आ रही किस्से-कहानियाँ। कंठस्थ करना = याद करना। नरो वा कुंजरों वा = हाथी या मनुष्य। मटकी = मिट्टी का बरतन। तर्क शिरोमणि = तर्क देने में सर्वश्रेष्ठ। सिर घुटाना = जड़ से बाल कटवाना। अकुंठित भाव से = संकोच के बिना। चूडाकर्म = सिर के बाल कटवाना। नापित = नाई। निष्पन्न = पूर्ण । वयोवृद्धता = बूढी उमर। अपमान = निरादर। मंथरता = धीमी गति। पटु = चतुर। पिंड छुड़ाना = पीछा छुड़वाना। अतिशयोक्तियाँ = बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें। अमरबेल = एक ऐसी लता जो बिना जड़ के होती है और वृक्षों से रस चूसकर फैलती है। प्रमाणित = प्रमाण से सिद्ध। आभा = प्रकाश, रोशनी। उद्भासित = प्रकाशित। पागुर = जुगाली। निस्तब्धता = शांति, चुप्पी। प्रशांत = पूरी तरह शांत। आतंकित = डरा हुआ। नाती = बेटी का पुत्र। अनुरोध = आग्रह। मचान = टाँड। विस्मित = हैरान । अमरौती खाकर आना = अमरता लेकर आना। विषमताएँ = कठिनाइयाँ, बाधाएँ। सम्मान = आदर। अपभ्रंश = भाषा का बिगड़ा हुआ रूप । अवज्ञा = आज्ञा न मानना। कारागार = जेल। आश्वासन = भरोसा। माई = माँ। विषम = विपरीत। बड़े लाट = गवर्नर जनरल । प्रतिद्धन्द्धियों = एक दूसरे के विपरीत लोग। दुर्लभ = कठिन।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
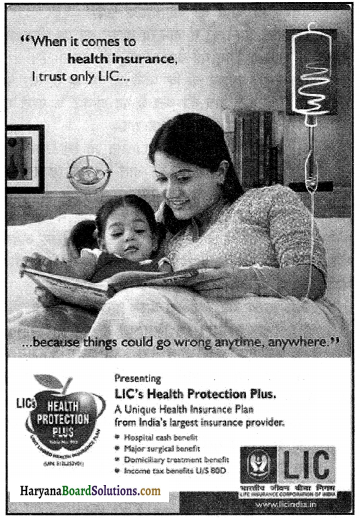
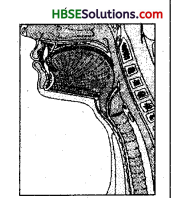
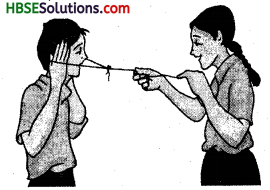

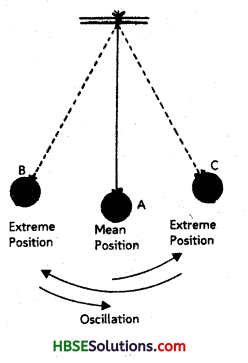
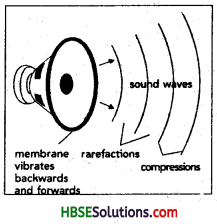 Sound reaches from one source to another. It travels from one point to another through some medium. Sound waves can travel through air, liquid and even through solids. What we hear one another, that sound travels through air medium. But we can bear some body talking in next room too, that means sound waves have crossed wall to reach us. Dolphins and whales communicate in water.
Sound reaches from one source to another. It travels from one point to another through some medium. Sound waves can travel through air, liquid and even through solids. What we hear one another, that sound travels through air medium. But we can bear some body talking in next room too, that means sound waves have crossed wall to reach us. Dolphins and whales communicate in water.