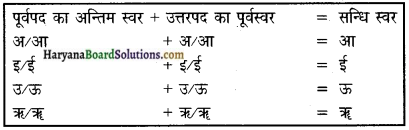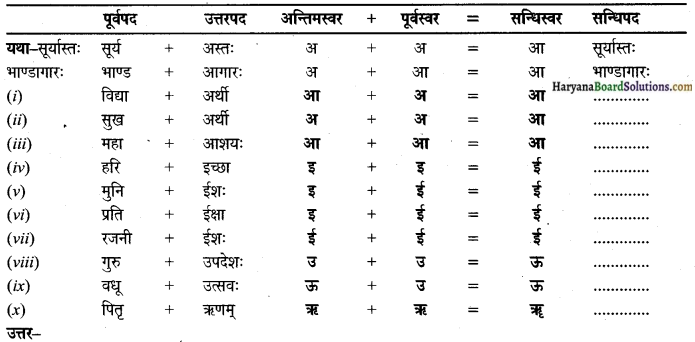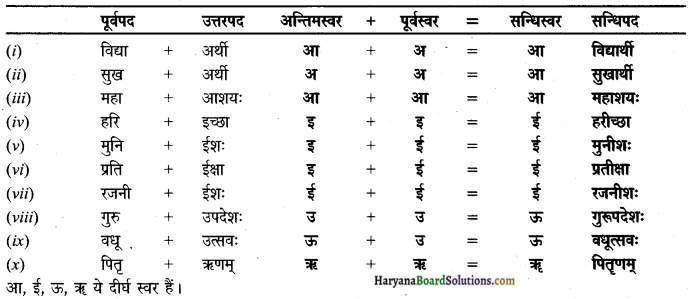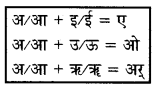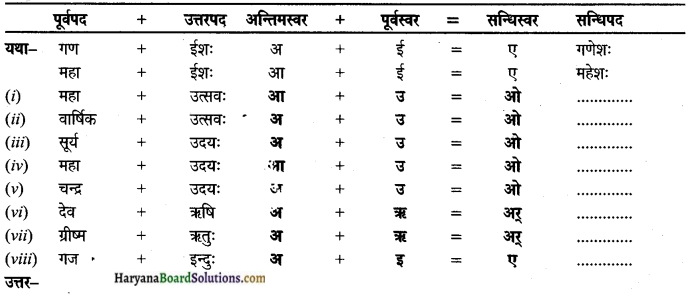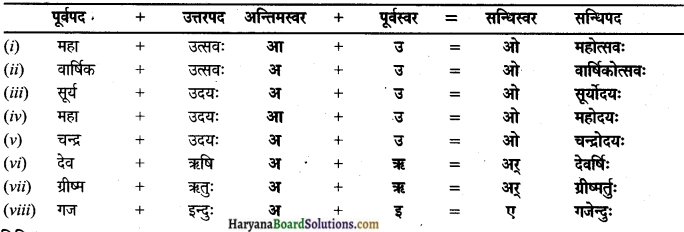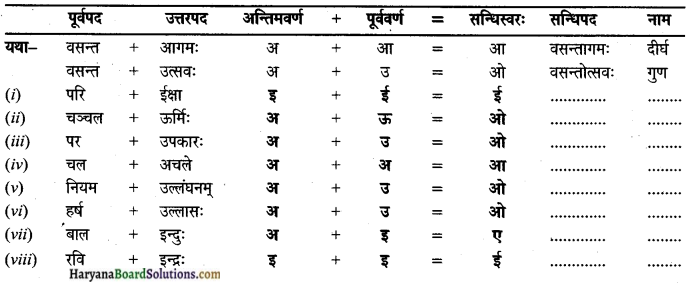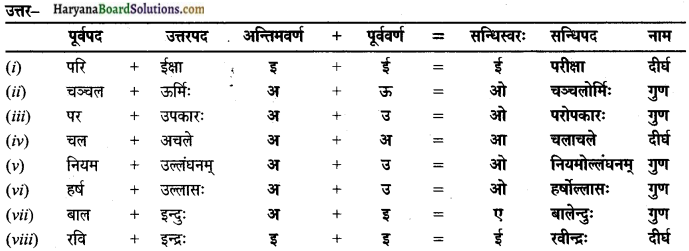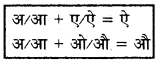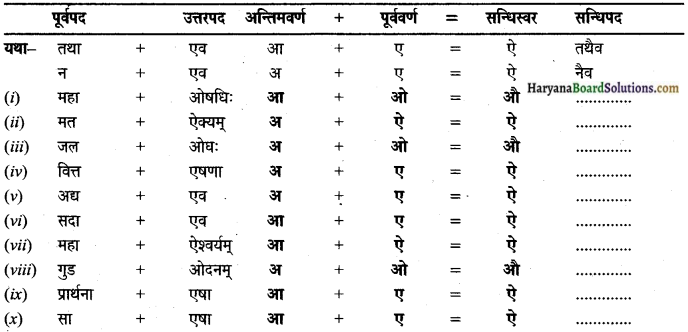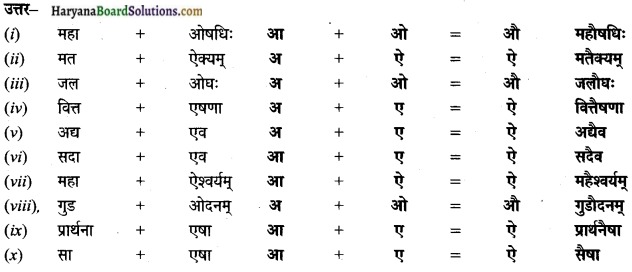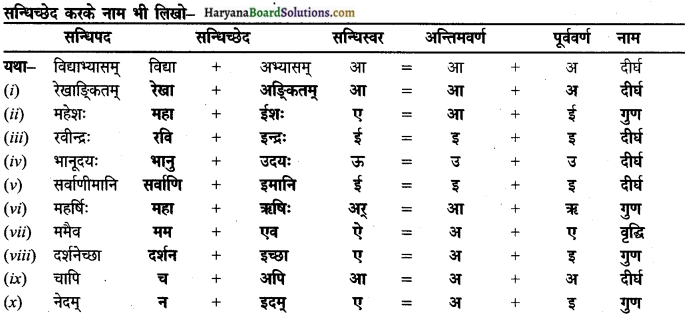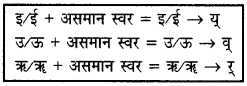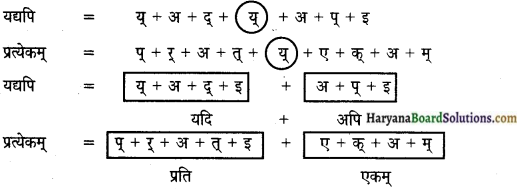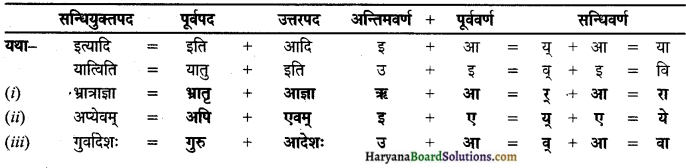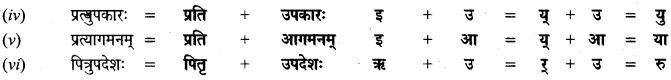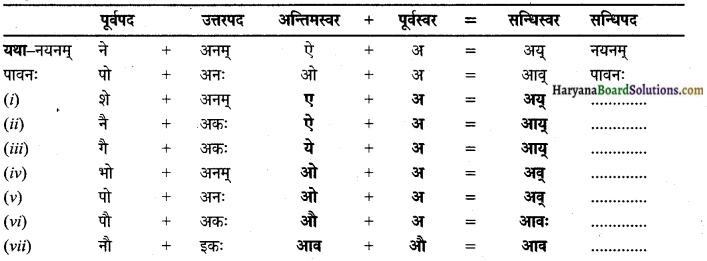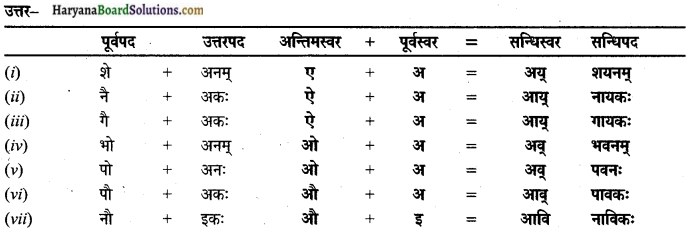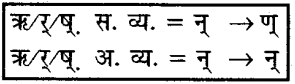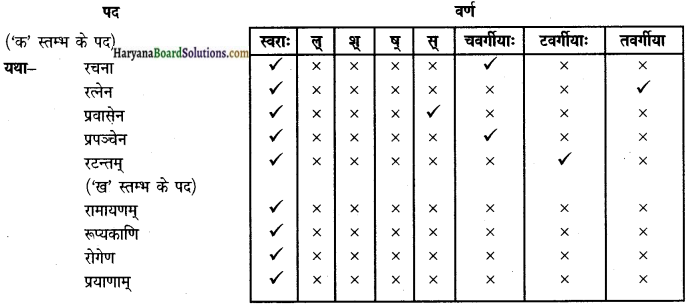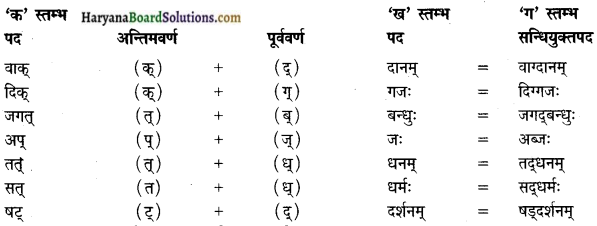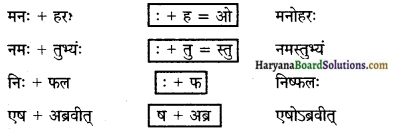Haryana State Board HBSE 9th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 1 दो बैलों की कथा Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 9th Class Hindi Solutions Kshitij Chapter 1 दो बैलों की कथा
HBSE 9th Class Hindi दो बैलों की कथा Textbook Questions and Answers
दो बैलों की कथा प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class Hindi प्रश्न 1.
कांजीहौस में कैद पशुओं की हाज़िरी क्यों ली जाती होगी ?
उत्तर-
कांजीहौस में कैद पशुओं की हाज़िरी इसलिए ली जाती होगी, ताकि उनमें से किसी पशु को कोई चुराकर न ले जाए। कांजीहौस में लाए गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी कांजीहौस के कर्मचारियों की ही होती थी।
पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class Hindi प्रश्न 2.
छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया ?
उत्तर-
एक सच्चाई है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति के दुख को अधिक अनुभव कर सकता है। गया के घर में छोटी बच्ची की विमाता हर समय उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि गया (छोटी बच्ची का पिता) अपने बैलों को अच्छा चारा देता है और झूरी के बैलों को रूखा-सूखा भूसा खाने को देता है और मारता भी है तो उनके प्रति गया के अन्याय को देखकर छोटी बच्ची के मन में प्रेम उमड़ आया था।
दो बैलों की कथा का प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class Hindi प्रश्न 3.
कहानी में बैलों के माध्यम से कौन-कौन से नीति-विषयक मूल्य उभरकर आए हैं ?
उत्तर-
प्रस्तुत कहानी में नीति संबंधी अनेक विषयों की…………. ओर संकेत किया गया है। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-
(क) अपने स्वामी के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए।
(ख) सच्चा मित्र वही होता है, जो हर सुख-दुःख में साथ रहे।
(ग) आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।
(घ) आजादी के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ता है।
(ङ) एकता में सदा बल होता है।
(च) परोपकार के लिए आत्मबलिदान देना महान् कार्य है।

दो बैलों की कथा प्रश्न उत्तर Class 9 HBSE Hindi प्रश्न 4.
प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ ‘मूर्ख’ का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है ?
उत्तर-
प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने गधे को ‘मूर्ख’ न कहकर उसकी अन्य स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख किया है, यथा-वह निरापद सहिष्णु होता है। यदि कोई उसको मारता है या दुर्व्यवहार करता है तो वह शांत स्वभाव से उसे सहन कर लेता है। उसका प्रतिरोध नहीं करता, जैसे अन्य पशु करते हैं। उसे कभी किसी बात पर क्रोध नहीं आता। वह सदा उदास व निराश ही दिखाई देता है। वह सुख-दुःख, हानि-लाभ सब स्थितियों में समभाव रहता है। अतः उसका सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए लोग उसे ‘मूर्ख’ की पदवी दे देते हैं।
दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class Hindi प्रश्न 5.
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी ? ।
उत्तर-
हीरा और मोती, दोनों सदा एक-दूसरे के सुख-दुःख में साथ देते थे। उदाहरणार्थ-जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया और हल जुआ आदि लेकर भाग गया और उन्हें तोड़ डाला और कहा कि यदि वह तुम पर हाथ उठाएगा तो मैं भी उसे गिरा दूंगा। इसी प्रकार जब दोनों को भारी-भरकम साँड़ का सामना करना पड़ा तो भी दोनों सच्चे मित्रों की भाँति उससे संघर्ष किया और उसे हरा दिया। इसी प्रकार जब मोती मटर के खेत में फंस गया था, हीरा ने वहाँ से न भागकर उसके साथ ही अपने आपको पकड़वा लिया। इसी प्रकार जब कांजीहौस में हीरा रस्सी से बँधा हुआ था, किन्तु मोती स्वतंत्र था। वह चाहता तो कांजीहौस से भाग सकता था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया और हीरा के साथ ही खड़ा रहा और कांजीहौस के चौकीदार से मार भी खाई। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।
दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class Hindi प्रश्न 6.
‘लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो।’-हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
मोती को यह देखकर कि गया की छोटी-सी बच्ची को गया की पत्नी (बच्ची की विमाता) खूब मारती व तंग करती है। वह गया की पत्नी को उठाकर पटकने की बात कहता है। यह सुनकर हीरा उपरोक्त शब्द कहता है। हीरा के इन शब्दों से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण एवं सम्मान की भावना रखते थे। वे मानते थे कि नारी को पीटना व मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। यह हमारी संस्कृति के भी विपरीत है।
प्रश्न 7.
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है ?
उत्तर-
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व्यक्त किया गया है। झूरी किसान है। उसके पास हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। वह अपने बैलों को अत्यधिक प्यार करता है। उनकी देखभाल भी भली-भाँति करता है। उन्हें अपने से दूर करने में उसका जी छोटा होता है, किन्तु उन्हें पुनः प्राप्त करके अत्यंत खुश होता है। उनसे गले लगकर मिलता है जैसे बिछुड़े हुए मित्र मिलते हैं। उसकी पत्नी भी अपनी गलती मानकर बैलों के माथे चूम लेती है। अतः स्पष्ट है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत निकटता एवं आत्मीयता के संबंधों के रूप में व्यक्त किया गया है।
प्रश्न 8.
“इतना तो हो ही गया कि नौ दस प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे।”-मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएँ बताइए।
उत्तर-
मोती भले ही स्वभाव का विद्रोही लगता हो, किन्तु वास्तव में वह एक सच्चा मित्र और पशु होते हुए भी मानवीय गुणों का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी उसे अन्याय या अत्याचार अनुभव होता है, वहीं वह अपना विद्रोह व्यक्त करता है। वह दूसरों के दुःखों को अनुभव करता है और उसे दूर करने के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। छोटी बच्ची के प्रति होने वाले अन्याय को देखकर वह कह उठता है कि “मालकिन को ही उठाकर पटक हूँ।” इसी प्रकार कांजीहौस में वह सींगों से दीवार को गिराकर अन्य पशुओं की जान बचा देता है। उसे इसके लिए बहुत मार खानी पड़ी और कसाई के हाथों नीलाम होना पड़ा, किन्तु उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी। वह चाहता है कि वह अधिक-से-अधिक दूसरों के काम आए।
प्रश्न 9.
आशय स्पष्ट कीजिए-
(क) अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
(ख) उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती; पर दोनों के हृदय को मानों भोजन मिल गया।
उत्तर-
(क) कहानीकार ने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हीरा और मोती के चरित्रों पर प्रकाश डाला है। इन दोनों बैलों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जिससे वे एक-दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ जाते थे। भले ही वह गया को मजा चखाने की योजना हो, साँड से भिड़ने की बात हो अथवा कांजीहौस में परोपकार करने में आत्मबलिदान की बात हो। इन सब घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक-दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ लेते थे। ऐसी शक्ति से अपने आपको प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य वंचित लगता है।
(ख) गया के घर में दोनों बैलों का अत्यधिक अनादर होता था, किन्तु गया की छोटी-सी बच्ची बैलों का सम्मान करती थी और घरवालों से चोरी-चोरी उन्हें एक रोटी रोज लाकर खिलाती थी। इतने बड़े-बड़े बैलों का एक-एक रोटी में कुछ नहीं बनता था, किन्तु सम्मान की दृष्टि से बैलों का मन संतुष्ट हो जाता था। उनसे भले ही उनकी भूख न मिट सके, किन्तु मन को यह यकीन हो जाता था कि यहाँ भी हमारा सम्मान करने वाला अवश्य है।
प्रश्न 10.
गया ने हीरा-मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि-
(क) गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था।
(ख) गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी।
(ग) वह हीरा-मोती के व्यवहार से बहुत दुःखी था।
(घ) उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी।
(सही उत्तर के आगे (√) का निशान लगाइए)
उत्तर-
(ग) वह हीरा-मोती के व्यवहार से बहुत दुःखी था।

रचना और अभिव्यक्ति
प्रश्न 11.
हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा-मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें।
उत्तर-
निश्चय ही यदि कोई व्यक्ति शोषण या अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ ऊँची करता है तो उसे सदा ही संघर्ष करना पड़ता है और अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। हीरा और मोती ने गया के द्वारा किए गए अन्याय तथा शोषण का विरोध किया तो उसने उन्हें भूखा रखा। इसी प्रकार कांजीहौस में कांजीहौस के मुँशी और पहरेदार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वहाँ भी उन्हें मार खानी पड़ी। अतः यह स्पष्ट है कि शोषण के विरुद्ध बोलने वाले को सदा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
प्रश्न 12.
क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है ?
उत्तर-
दो बैलों की कथा’ शीर्षक कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अत्यधिक सीधे और सरल हैं इसलिए अंग्रेज सरकार उनका शोषण करती है और उनके जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता से वंचित रखना चाहती थी। प्रेमचंद ने दोनों बैलों के चरित्र के माध्यम से यह समझाया है कि यदि हम बैलों की भाँति एकता बनाकर संघर्ष करेंगे तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। यदि आपस में झगड़ते रहे तो कभी आजाद नहीं हो सकेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बार-बार संघर्ष करना पड़ता है। अतः यह कहानी भारत की आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करने वाली कहानी है।
भाषा-अध्ययन
प्रश्न 13.
बस इतना ही काफी है।
फिर मैं भी ज़ोर लगाता हूँ
‘ही’, ‘भी’ वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी
में से पाँच ऐसे वाक्य छाँटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो।
उत्तर-
(क) फिर भी बदनाम हैं।
(ख) कभी-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है।
(ग) कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे।
(घ) मालकिन मुझे मार ही डालेगी।
(ङ) पीछे से तुम भी उन्हीं की-सी कहोगे।
प्रश्न 14.
रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छाँटकर उसके भी भेद लिखिए
(क) दीवार का गिरना था कि अधमरे-से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे।
(ख) सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आँखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया।
(ग) हीरा ने कहा-गया के घर से नाहक भागे।
(घ) मैं बेचूंगा, तो बिकेंगे।
(ङ) अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे-मारे न छोड़ता।
उत्तर-
(क) मिश्र वाक्य
दीवार का गिरना था। (प्रधान उपवाक्य)
अधमरे-से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। (संज्ञा उपवाक्य)
(ख) मिश्र वाक्य
जिसकी आँखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। (विशेषण उपवाक्य)
सहसा एक दढ़ियल आदमी आया। (प्रधान वाक्य)
(ग) मिश्र वाक्य
हीरा ने कहा। (प्रधान वाक्य)
गया के घर से नाहक भागे। (संज्ञा उपवाक्य)
(घ) मिश्र वाक्य
मैं बेचूँगा। (प्रधान वाक्य)
तो बिकेंगे। (क्रिया-विशेषण उपवाक्य)

(ङ) मिश्रवाक्य –
अगर वह मुझे पकड़ता। (प्रधान वाक्य)
मैं बे-मारे न छोड़ता। (क्रियाविशेषण उपवाक्य)
प्रश्न 15.
कहानी में जगह-जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई पाँच मुहावरे छाँटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
उत्तर-
- ईंट का जवाब पत्थर से देना-भारतवर्ष शांतिप्रिय अवश्य है, किन्तु ईंट का जवाब पत्थर से देना भी भली-भाँति जानता है।
- दाँतों पसीना आना-पी०एच०डी० की उपाधि प्राप्त करने के लिए तो दाँतों पसीना आ जाता है।
- कोई कसर न उठा रखना-मैंने परीक्षा में प्रथम आने में कोई कसर न उठा रखी थी।
- मज़ा चखाना-मोती और हीरा ने मिलकर साँड को खूब मजा चखाया था।
- जान से हाथ धोना-मोहन को चरस बेचने के धंधे में जान से हाथ धोने पड़े।
पाठेतर सक्रियता
पशु-
पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएँ ढूँढकर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए।
उत्तर-
यह प्रश्न परीक्षोपयोगी नहीं है।
HBSE 9th Class Hindi दो बैलों की कथा Important Questions and Answers
प्रश्न 1.
‘दो बैलों की कथा’ नामक कहानी का उद्देश्य लिखिए।
उत्तर-
‘दो बैलों की कथा’ शीर्षक कहानी एक सोद्देश्य रचना है। इस कहानी में लेखक ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। कहानी में बताया गया है कि स्वतंत्रता सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए बार-बार प्रयास किया जाता है। स्वामी के प्रति वफादारी निभाने का वर्णन करना कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। कहानीकार का सच्ची मित्रता पर प्रकाश डालना भी एक उद्देश्य है। एक सच्चा मित्र ही सुख-दुःख में साथ देता है। आत्म रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए। ‘एकता में सदा बल है’ इस सर्वविदित सत्य को दर्शाना भी कहानी का मूल उद्देश्य है।
प्रश्न 2.
‘दो बैलों की कथा’ कहानी के अनुसार बताइए कि आज संसार में किन लोगों की दुर्दशा हो रही है और क्यों?
उत्तर-
‘दो बैलों की कथा’ नामक कहानी में बताया गया है कि आज सीधे-सादे व साधारण लोगों की दुर्दशा हो रही है। इस संसार में सरलता, सीधापन, सहनशीलता आदि गुणों का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। सरलता को मूर्खता और सहनशीलता को डरपोक होना समझा जाता है। आज इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति का शोषण होता है। आज हर सीधे-सादे व्यक्ति का शोषण किया जाता है। आज शक्तिशाली व चालाक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है। उससे सभी लोग डरते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रश्न उठाया है कि अफ्रीका व अमेरिका में भारतीयों का सम्मान क्यों नहीं है ? स्वयं ही इसका उत्तर देते उसने कहा है, क्योंकि वे सीधे-सादे
और परिश्रमी हैं। वे चोट खाकर भी सब कुछ सहन कर जाते हैं। इसके विपरीत जापान ने युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया में अपना सम्मान अर्जित कर लिया है।
प्रश्न 3.
‘हीरा और मोती सच्चे मित्रों के आदर्श हैं’ कैसे?
उत्तर-
सच्चे मित्र एक-दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। वे एक-दूसरे के लिए त्याग भी करते हैं और एक साथ खाते-पीते भी हैं। ये सभी गुण हीरा और मोती दोनों बैलों में भी देखे जा सकते हैं। हीरा और मोती एक-दूसरे से प्यार करते हैं। एक-दूसरे को चाट-चूमकर और सूंघकर अपने प्यार का प्रदर्शन करते हैं। वे आपस में कौल-क्रीड़ा, शरारत आदि भी करते हैं। हीरा-मोती गहरे मित्र हैं। वे इकट्ठे खाते-पीते, खेलते व एक-दूसरे से सींग भिड़ाते हैं। वे एक-दूसरे को संकट से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। इससे पता चलता है कि हीरा-मोती बैल होते हुए भी सच्चे मित्रों के आदर्श हैं।
प्रश्न 4.
प्रस्तुत कहानी के आधार पर मोती के चरित्र पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
कहानी में मोती एक बैल है। वह कुछ गर्म स्वभाव वाला है। वह स्वामिभक्त है। वह अन्याय करने वाले का विरोध करता है। झूरी का साला गया जब उनके प्रति अन्याय एवं अत्याचार करता है तो मोती उसका हल-जुआ लेकर भाग जाता है। मोती कहता भी है कि “मुझे मारेगा तो उठाकर पटक दूंगा।” जब गया उसका अपमान करता है और मारता है तो वह हीरा से कहता है कि “एकाध को सींगों पर उठाकर फैंक दूंगा।” इसी प्रकार वह दढ़ियल कसाई को भी सींग दिखाकर गाँव से भगा देता है। किन्तु वह दुखियों के प्रति दया का भाव भी रखता है। वह गया की बेटी तथा कांजीहौस में फँसे हुए जानवरों के प्रति दया दिखाता है।
प्रश्न 5.
‘हीरा एक धैर्यशील एवं अहिंसक प्राणी है’-पठित कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए।
उत्तर-
कहानी को पढ़कर लगता है कि हीरा गांधीवादी विचारधारा का समर्थक है। वह मुसीबत के समय धैर्य बनाए रखता है। उसे पता है कि धैर्य खो देने से काम बिगड़ जाता है। वह कदम-कदम पर अपने मित्र मोती को भी धैर्य से काम लेने का परामर्श देता है। जब गया बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था तो मोती ने दो बार गया को गाड़ी सहित सड़क की खाई में गिराना चाहा, किन्तु हीरा ने उसे संभाल लिया। इसी प्रकार गया जब बैलों के प्रति अन्याय करता है, और उन्हें सूखा भूसा देता है तो भी मोती को गुस्सा आ जाता है और वह उससे बदला लेने की ठान लेता है। वह उसे मार गिराना चाहता है। उस समय हीरा ने ही उसे रोक लिया था, गया की पत्नी को भी मोती सबक सिखाना चाहता था, किन्तु हीरा ने कहा कि स्त्री जाति पर हाथ उठाना या सींग चलाना मना है, यह क्यों भूल जाता है। हीरा के धैर्य की परीक्षा तो उस समय होती है जब कांजीहौस की दीवार तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है। उसे मोटी रस्सी में बाँध दिया जाता है। वह कहता है कि जोर तो मारता ही जाऊँगा चाहे कितने ही बँधन क्यों न पड़ जाएँ? इन सब तथ्यों से पता चलता है कि हीरा एक धैर्यशील बैल था।

प्रश्न 6.
साँड के साथ बैलों की टक्कर की घटना से हमें क्या उपदेश मिलता है ?
अथवा
साँड को मार गिराने की घटना के माध्यम से लेखक क्या उपदेश देना चाहता है ?
उत्तर-
प्रस्तुत कहानी में बैलों द्वारा साँड को हरा देने की घटना के पीछे एक महान संदेश छिपा हुआ है। इस घटना के माध्यम से लेखक ने संगठित होकर शत्रु का मुकाबला करने की प्रेरणा दी है। उसने बताया है जिस प्रकार हीरा और मोती दो बैल शक्तिशाली साँड को मार भगाते हैं, उसी प्रकार भारतीय भी आपसी मतभेद को त्यागकर एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर कर सकते हैं। अतः लेखक ने ‘एकता में बल है’ नीति वाक्य को भी इस घटना के माध्यम से सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है।
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
‘दो बैलों की कथा’ पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है ?
(A) कविता
(B) निबंध
(C) एकांकी
(D) कहानी
उत्तर-
(D) कहानी
प्रश्न 2.
‘दो बैलों की कथा’ कहानी के लेखक कौन हैं ?
(A) हज़ारीप्रसाद द्विवेदी
(B) प्रेमचंद
(C) महादेवी वर्मा
(D) जाबिर हुसैन
उत्तर-
(B) प्रेमचंद
प्रश्न 3.
प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे ?
(A) कविता
(B) उपन्यास
(C) एकांकी
(D) निबंध
उत्तर-
(B) उपन्यास
प्रश्न 4.
प्रेमचंद ने अपनी कहानी ‘दो बैलों की कथा’ में किसका वर्णन किया है ?
(A) विद्यार्थियों का
(B) पक्षियों का
(C) बैलों की मित्रता का
(D) किसान का
उत्तर-
(C) बैलों की मित्रता का
प्रश्न 5.
‘दो बैलों की कथा’ कहानी में किस-किस का संबंध दिखाया गया है ?
(A) किसान और उसके पशुओं का
(B) किसान और महाजन का
(C) महाजन और पशुओं का
(D) इनमें से किसी का नहीं
उत्तर-
(A) किसान और उसके पशुओं का
प्रश्न 6.
लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है ?
(A) बैल को
(B) गाय को
(C) भैंस को
(D) गधे को
उत्तर-
(D) गधे को

प्रश्न 7.
हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं ?
(A) बैल
(B) कुत्ता
(C) गधा
(D) ऊँट
उत्तर-
(C) गधा
प्रश्न 8.
गाय किस दशा में सिंहनी का रूप धारण कर लेती है ?
(A) बैठी हुई
(B) दौड़ती हुई
(C) चरती हुई
(D) ब्याही हुई
उत्तर-
(D) ब्याही हुई
प्रश्न 9.
गधे के चेहरे पर कौन-सा स्थायी भाव सदा छाया रहता है ?
(A) प्रसन्नता का
(B) असंतोष का
(C) विषाद का
(D) निराशा का
उत्तर-
(C) विषाद का
प्रश्न 10.
भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था ?
(A) अमेरिका
(B) इंग्लैंड
(C) जर्मनी
(D) अफ्रीका
उत्तर-
(A) अमेरिका
प्रश्न 11.
किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिला दिया ?
(A) भारत
(B) जापान
(C) अमेरिका
(D) इंग्लैंड
उत्तर-
(B) जापान
प्रश्न 12.
“अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते” ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे हैं ?
(A) भारतीयों के लिए
(B) जापान के लोगों के लिए
(C) पाकिस्तान के लोगों के लिए
(D) चीन के लोगों के लिए
उत्तर-
(A) भारतीयों के लिए
प्रश्न 13.
‘बछिया का ताऊ’ किसके लिए प्रयोग किया जाता है ?
(A) शेर के
(B) हाथी के
(C) भैंसा के
(D) बैल के
उत्तर-
(D) बैल के
प्रश्न 14.
हीरा और मोती बैलों के स्वामी का क्या नाम था ?
(A) किश्न
(B) झूरी
(C) होरी
(D) रामेश्वर
उत्तर-
(B) झूरी
प्रश्न 15.
झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे ?
(A) पछाईं
(B) राजस्थानी
(C) मूर्रा
(D) जंगली
उत्तर-
(A) पछाईं

प्रश्न 16.
झूरी के साले का क्या नाम था ?
(A) मोहन
(B) गया
(C) बृज
(D) किश्न
उत्तर-
(B) गया
प्रश्न 17.
दोनों बैल कौन-सी भाषा में एक-दूसरे के भावों को समझ लेते थे ?
(A) मूक भाषा
(B) सांकेतिक भाषा
(C) संगीतात्मक भाषा
(D) रंभाकर
उत्तर-
(A) मूक भाषा
प्रश्न 18.
झूरी ने प्रातः ही नाद पर खड़े बैलों को देखकर क्या किया ?
(A) बैलों को पीटा
(B) उन्हें गले से लगा लिया
(C) घर से निकाल दिया
(D) बेच दिया
उत्तर-
(B) उन्हें गले से लगा लिया
प्रश्न 19.
“कैसे नमकहराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया” ये शब्द किसने कहे ?
(A) गया ने
(B) झूरी की पत्नी ने
(C) झूरी ने
(D) झूरी की बेटी ने
उत्तर-
(B) झूरी की पत्नी ने
प्रश्न 20.
“वे लोग तुम जैसे बुद्धओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं” ये शब्द किसने किसके प्रति कहे ?
(A) झूरी की पत्नी ने झूरी को
(B) गया ने झूरी के प्रति
(C) गया की बेटी ने गया को
(D) इनमें से किसी ने नहीं
उत्तर-
(A) झूरी की पत्नी ने झूरी को
प्रश्न 21.
दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया ?
(A) पीटता हुआ
(B) बैलगाड़ी में जोतकर
(C) हल में जोतकर
(D) प्रेमपूर्वक
उत्तर-
(B) बैलगाड़ी में जोतकर
प्रश्न 22.
गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों थी ?
(A) उसकी माँ मर चुकी थी
(B) सौतेली माँ मारती थी
(C) उसे दोनों बैल सुंदर लगते थे
(D) वह किसी को भूखा नहीं देख सकती थी
उत्तर-
(B) सौतेली माँ मारती थी
प्रश्न 23.
गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ किसने खोली थी ?
(A) गया की पत्नी ने
(B) गया के नौकर ने
(C) गया की बेटी ने
(D) स्वयं गया ने
उत्तर-
(C) गया की बेटी ने
प्रश्न 24.
हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया था ?
(A) वह बीमार थी
(B) वह दयालु थी
(C) वह स्त्री जाति थी
(D) वह बूढ़ी थी
उत्तर-
(C) वह स्त्री जाति थी
प्रश्न 25.
“गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए” ये शब्द किसने कहे थे ?
(A) हीरा ने
(B) मोती ने
(C) साँड ने
(D) झूरी ने
उत्तर-
(A) हीरा ने
प्रश्न 26.
खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था ?
(A) जेल में
(B) अपने घर में
(C) कांजीहौस में
(D) थाने में
उत्तर-
(C) कांजीहौस में
प्रश्न 27.
‘दीवार को तोड़ना’ से बैलों की कौन-सी भावना का बोध होता है ?
(A) अनुशासन
(B) विद्रोह
(C) दया
(D) घृणा
उत्तर-
(B) विद्रोह
प्रश्न 28.
मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर भी कौन-सा जानवर नहीं भागा ?
(A) घोड़ी
(B) बकरी
(C) भैंस
(D) गधा
उत्तर-
(D) गधा
प्रश्न 29.
कांजीहौस से हीरा और मोती को किसने खरीदा?
(A) सड़ियल ने
(B) दड़ियल ने
(C) मुच्छड़ ने
(D) अड़ियल ने
उत्तर-
(B) दड़ियल ने

दो बैलों की कथा प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या/भाव ग्रहण
1. जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दरजे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, व्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है; किन्तु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब, सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी।[पृष्ठ 5]
शब्दार्थ-बुद्धिहीन = मूर्ख । परले दरजे का बेवकूफ = अत्यधिक मूर्ख । निरापद = कष्ट न पहुँचाने की भावना। सहिष्णुता = सहनशीलता। पदवी = उपाधि। अनायास = अचानक। क्रोध = गुस्सा। असंतोष की छाया = संतोषहीनता का भाव।
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिन्दी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग-1 में संकलित ‘दो बैलों की कथा’ शीर्षक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक महान् कथाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। इस कहानी में लेखक ने दो बैलों की कहानी के माध्यम से भारतीय जीवन-मूल्यों पर प्रकाश डाला है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि गधे के सीधेपन के कारण ही उसे गधा, मूर्ख कहा जाता है। वस्तुतः लेखक ने ‘गधा’ शब्द पर व्यंग्य करते हुए ये शब्द कहे हैं
व्याख्या/भाव ग्रहण-लेखक ने बताया है कि सब जानवरों व पशुओं में गधा ही सीधा एवं सरल पशु है। वह सबसे अधिक नासमझ पशु है। अपने सीधेपन और मंद-बुद्धि के कारण उसका सर्वत्र अपमान होता है। समाज में जब किसी को परले दरजे का मूर्ख कहा जाता है तो उसे ‘गधा’ शब्द से संबोधित करते हैं। सीधेपन, बुद्धिहीनता, सहनशीलता आदि गुणों के कारण उसे यह उपाधि (गधा) मिली है। गधे में अधिकार-बोध की भावना तनिक भी नहीं होती। न उसमें विद्रोह की भावना है और न अधिकारचेष्टा ही। वह एक सहनशील प्राणी है, जो हर प्रकार के कष्टों को चुपचाप सहन कर लेता है। गाय भी सींग मारती है, भले ही उसे लोग गाय माता कहते हों, किन्तु वह जब ब्याई हुई होती है तो अचानक ही शेरनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ तक कि कुत्ते को भी लोग गरीब कहते हैं, किन्तु उसे भी कभी-न-कभी गुस्सा आ ही जाता है। किन्तु गधे जी को कभी गुस्सा करते न देखा होगा और न सुना होगा। उससे जितना चाहे काम लो, जितना चाहे पीट लो, और तो और चाहे सड़ी-गली व सूखी घास भी डाल दो तो भी उसके चेहरे पर कभी असंतोष की झलक दिखाई नहीं देगी।
विशेष-
- ‘गधा’ शब्द की अनेक अर्थों में सुंदर व्यंजना की गई है।
- ‘गधा’ शब्द को मूर्खता का पर्याय सिद्ध किया गया है।
- अन्य पशुओं से गधे की तुलना करके कहानीकार ने गधे की मूर्खता को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है।
- भाषा सरल एवं सुबोध है।
उपर्युक्त गयांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(1) हम किसी व्यक्ति को गधा क्यों कहते हैं ?
(2) गधे के जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है ?
(3) ‘परले दरजे का बेवकूफ’ से क्या अभिप्राय है ?
(4) गधे को गधा क्यों कहा जाता है ?
उत्तर-
(1) जब हम किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना चाहते हैं, तब ही उसे गधा कहते हैं।
(2) सीधापन ही गधे के जीवन की प्रमुख विशेषता है।
(3) ‘परले दरजे का बेवकूफ’ से अभिप्राय है-पूर्णतः मूर्ख व्यक्ति, जिसे दीन-दुनिया की कोई खबर न हो।
(4) गधे की अत्यधिक सहनशीलता, सरलता, अक्रोधी स्वभाव, असंतोष को व्यक्त न करना एवं सुख-दुःख में सदा समान रहने के कारण ही उसे गधा कहते हैं। दूसरे जानवर ऐसे नहीं होते, वे क्रोध भी करते हैं और असंतोष भी दिखाते हैं।
2. उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख-दुख, हानि-लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों-मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। [पृष्ठ 5]
शब्दार्थ-विषाद = दुःख। दशा = हालत। पराकाष्ठा = चरम सीमा। बेवकूफ = मूर्ख । अनादर = अपमान। सीधापन = सरलता।
प्रसंग-प्रस्तुत गद्यावतरण हिन्दी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग-1 में संकलित प्रेमचंद की कहानी ‘दो बैलों की कथा’ से अवतरित किया गया है। इसमें लेखक ने गधे के सीधेपन का व्यंग्यार्थ के रूप में चित्रण किया है। आज के युग में सीधा या साधारण व सरल हृदयी होना मूर्खता कहलाता है। इन शब्दों में यही भाव झलकता है।
व्याख्या/भाव ग्रहण-प्रेमचंद गधे के स्वभाव का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि गधा स्वभाव से सीधा होता है। उसमें किसी प्रकार का छल-कपट नहीं होता और न ही कभी प्रसन्नता की झलक ही दिखाई देती है। उसके चेहरे पर सदा निराशा का भाव ही छाया रहता है। सुख-दुःख, हानि-लाभ, सभी दशाओं में यह विषाद उसके चेहरे पर स्थायी रूप से छाया रहता है। ऐसा लगता है मानों ऋषि-मुनियों के सभी श्रेष्ठ गुण पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। इन्हीं श्रेष्ठ गुणों के कारण ही आदमी उसे ‘बेवकूफ’ कहता है। यह उसके सद्गुणों का अनादर है। ऐसा लगता है कि गधे का सीधापन उसके लिए अभिशाप है। अति सरलता के कारण संसार के लोग उस पर टीका-टिप्पणी करते हैं।
विशेष-
- गधे के सीधेपन को व्यंग्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका अत्यधिक सीधापन ही उसकी मूर्खता बन गया है।
- कहानीकार ने गधे के वर्णन के माध्यम से सीधे-सादे व्यक्तियों को मूर्ख समझकर उनका शोषण करने वाले चालाक लोगों पर करारा व्यंग्य किया है।
- भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है।
- ‘सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं’ का अभिप्राय है, संसार में सदा टेढ़ा बनकर ही रहना चाहिए।’
- विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(1) प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए।
(2) लेखक के अनुसार गधे और ऋषि-मुनियों में कौन-सी समानताएँ हैं ?
(3) प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या संदेश दिया है ?
(4) स्थायी विषाद का अर्थ स्पष्ट करें।
उत्तर-
(1) प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि कुछ ही क्षणों या अवसरों को छोड़कर गधे के जीवन में सदा निराशा व दुःख ही छाया रहता है। ऋषि-मुनियों की भाँति सुख-दुःख में वह सदा समभाव रहता है। गधा सरल हृदय होता है। इतना कुछ होते हुए भी संसार गधे को मूर्ख कहता है। संसार में सीधापन उचित नहीं है।
(2) लेखक ने गधे और ऋषि-मुनियों की समानताएँ बताते हुए कहा है कि गधा और ऋषि-मुनि दोनों ही सरल स्वभाव वाले होते हैं। वे सुख-दुःख में सदा एक समान रहते हैं। वे अत्यधिक सहनशील और संतोषी होते हैं। उन्हें क्रोध भी बहुत कम आता है।
(3) प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने हमें संदेश दिया है कि हमें अत्यधिक सरल, सीधा व सहनशील नहीं होना चाहिए। हमें अत्याचार, अन्याय आदि के प्रति असंतोष प्रकट करना चाहिए और उसका विरोध भी करना चाहिए।
(4) चेहरे पर सदा छाई रहने वाली निराशा को ही लेखक ने स्थायी विषाद कहा है।
उपर्युक्त गयांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(1) हम किसी व्यक्ति को गधा क्यों कहते हैं ?
(2) गधे के जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है ?
(3) ‘परले दरजे का बेवकूफ’ से क्या अभिप्राय है ?
(4) गधे को गधा क्यों कहा जाता है ?
उत्तर-
(1) जब हम किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना चाहते हैं, तब ही उसे गधा कहते हैं।
(2) सीधापन ही गधे के जीवन की प्रमुख विशेषता है।
(3) ‘परले दरजे का बेवकूफ’ से अभिप्राय है-पूर्णतः मूर्ख व्यक्ति, जिसे दीन-दुनिया की कोई खबर न हो।
(4) गधे की अत्यधिक सहनशीलता, सरलता, अक्रोधी स्वभाव, असंतोष को व्यक्त न करना एवं सुख-दुःख में सदा समान रहने के कारण ही उसे गधा कहते हैं। दूसरे जानवर ऐसे नहीं होते, वे क्रोध भी करते हैं और असंतोष भी दिखाते हैं।
3. लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है ‘बैल’। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते-जुलते अर्थ में ‘बछिया के ताऊ’ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे; मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। [पृष्ठ 6]
शब्दार्थ-गधा = मूर्ख । बछिया का ताऊ = सीधा-सादा, भोंदू। बेवकूफी = मूर्खता। सर्वश्रेष्ठ = सबसे उत्तम। . प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिन्दी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग-1 में संकलित एवं महान् कथाकार प्रेमचंद कृत ‘दो बैलों की कथा’ शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कहानीकार ने गधे और बैल के गुणों की तुलना करते हुए बैल को गधे से बेहतर बताया है तथा ‘बछिया के ताऊ’ की सुंदर व्याख्या की है।
व्याख्या/भाव ग्रहण-लेखक ने गधे और बैल के प्रसंग के माध्यम से मनुष्य के कम या अधिक गुणों के आधार पर समाज में उसके स्थान व सम्मान की ओर संकेत किया है। ‘गधा’ शब्द का व्यंजनामूलक अर्थ है-मूर्ख। जब किसी व्यक्ति को अव्वल दरजे का मूर्ख कहना हो, तो उसे गधा कहा जाता है। सामान्यतः बैल को ‘बछिया का ताऊ’ कहा जाता है। यह शब्द भी मूर्खता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुछ लोग बैल को गधे से ज्यादा मूर्ख मानते हैं, लेकिन लेखक की मान्यता है कि बैल गधे से अधिक मूर्ख नहीं है। बैल में अपने अपमान का बदला लेने की भावना होती है। बैल में गधे की अपेक्षा अधिक संवेदना होती है। अतः बैल गधे की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है।
विशेष-
- लेखक ने समाज के सरल एवं सीधे-सादे लोगों के स्वभाव की व्यंग्यार्थ विवेचना की है।
- ‘बछिया का ताऊ’ मुहावरे का व्यंजनामूलक अर्थों में सुंदर विश्लेषण किया गया है। किसी को कम मूर्ख कहना हो तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है।
- भाषा सरल, सुबोध एवं मुहावरेदार है।
- वाक्य-योजना सरल एवं सार्थक है। – उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(1) गधे का छोटा भाई किसे बताया गया है और क्यों ?
(2) ‘बछिया का ताऊ’ किसे कहा जाता है और क्यों ?
(3) लेखक के अनुसार बैल का स्थान गधे से नीचा क्यों है ?
(4) बैल कैसा व्यवहार करता है ?
उत्तर-
(1) गधे का छोटा भाई बैल को बताया गया है क्योंकि जो गुण गधे में होते हैं, वे ही गुण कुछ कम मात्रा में बैल में भी पाए जाते हैं।
(2) बैल को ही ‘बछिया का ताऊ’ कहा जाता है। बछिया अर्थात गाय जो सरल और सीधी होती है। बैल में ये गुण उससे अधिक होते हैं। वह सरल, सीधा एवं कार्यशील होता है। अतः अत्यधिक सरलता और सीधेपन के कारण उसे ‘बछिया का ताऊ’ कहा जाता है।
(3) बैल कभी-कभी सहनशीलता छोड़कर क्रोध में सींग चला देता है। वह असंतोष भी प्रकट करता है तथा अपने अनुकूल व्यवहार न होने पर कभी-कभी अड़ भी जाता है। इसलिए उसका स्थान सीधेपन में गधे से नीचा है।
(4) बैल स्वभावतः सरल, सीधा एवं परिश्रमी होता है, किन्तु कभी-कभी दूसरों को मारता है, अड़ियलपन पर उतर आता है तथा अपना विरोध भी प्रकट करता है।
4. दोनों आमने-सामने या आस-पास बैठे हुए एक-दूसरे से मूक-भाषा में विचार-विनिमय करते थे। एक, दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक-दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे-विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल-धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हलकी-सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। [पृष्ठ 6]
शब्दार्थ-मूक-भाषा = मौन-भाषा। विनिमय = आदान-प्रदान। वंचित = रहित। विग्रह = मतभेद। विनोद = मज़ाक। आत्मीयता = अपनेपन। घनिष्ठता = गहन । फुसफुसी = हलकी, कच्ची।

प्रसंग-प्रस्तुत गद्यांश हिन्दी की पाठ्यपुस्तक ‘क्षितिज’ भाग-1 में संकलित प्रेमचंद की कहानी ‘दो बैलों की कथा’ से लिया गया है। लेखक ने इन पंक्तियों में हीरा-मोती की आपसी मित्रता की गहनता, आत्मीयता और प्रेमभाव को सुंदर ढंग से दर्शाया है। साथ ही पक्की दोस्ती के लक्षण की ओर भी संकेत किया है।
व्याख्या/भाव ग्रहण-लेखक का कथन है कि हीरा और मोती, दोनों बैलों के बीच अद्भुत मित्रता थी। दोनों आमने-सामने बैठकर मूक-भाषा में अपने हृदय की भावना व्यक्त करते थे। वे एक-दूसरे के मन की बात कैसे समझ पाते थे-यह बताना कठिन है। उनमें एक गुप्त शक्ति थी, जिसे आत्मीयता कहते हैं। इसी शक्ति के कारण उनके हृदय आपस में जुड़े हुए थे। प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य में इस शक्ति का अभाव है। लेखक ने हीरा और मोती की दोस्ती के विषय में बताया है कि दोनों एक-दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। चाटना, चूमना व सूंघना ही जानवरों के पास अपने प्रेम या स्वामिभक्ति को व्यक्त करने का साधन है, किन्तु हीरा और मोती कभी-कभी सींग भी भिड़ाते थे। ऐसा वे शत्रुता या नाराज़गी के कारण नहीं, अपितु हँसी-मजाक में ही करते थे। इससे उनकी आत्मीयता का भाव भी व्यक्त होता था। फिर दोस्ती में धक्का-मुक्का धौल-धप्पा तो चलता ही है। इसके अभाव में दोस्ती में बनावटीपन व हल्कापन रहता है। ऐसी दोस्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कहने का भाव है कि जहाँ आत्मीयता, सरलता, स्पष्टता, हँसी-मज़ाक आदि सब कुछ होता है, वहीं दोस्ती में गहनता होती है।
विशेष-
- लेखक ने हीरा और मोती की दोस्ती का वर्णन किया है।
- पशुओं की मूक भाषा की ओर संकेत किया गया है।
- भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। – उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर
प्रश्न-
(1) मोती और हीरा दोनों परस्पर किस भाषा में विचार-विमर्श करते थे ?
(2) उनमें कौन-सी शक्ति होने की बात कही है ?
(3) दोनों बैल अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे ?
(4) कैसी दोस्ती पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता ? ।
उत्तर-
(1) मोती और हीरा दोनों बैल मूक-भाषा में विचार-विमर्श करते थे।
(2) लेखक ने दोनों बैलों के बीच किसी गुप्त शक्ति के होने की बात कही है।
(3) दोनों बैल एक-दूसरे को चाटकर अथवा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे।
(4) फुसफुसी व हल्की दोस्ती में अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता।
दो बैलों की कथा Summary in Hindi
दो बैलों की कथा लेखक-परिचय
प्रश्न-
मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी कहानी-कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
अथवा
मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए।
उत्तर-
1. जीवन-परिचय-मुंशी प्रेमचंद एक महान् कथाकार थे। उन्हें उपन्यास-सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म सन् 1880 में बनारस के निकट लमही नामक गाँव के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपतराय था। पाँच वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। विमाता (सौतेली माँ) का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। 14 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात् परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के दौरान ही प्रेमचंद जी डिप्टी-इंस्पैक्टर के पद तक पहुँचे। वे स्वभाव से स्वाभिमानी थे। सन् 1928 में प्रेमचंद जी नौकरी से त्याग-पत्र देकर गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने जीवन-पर्यन्त साहित्य-सेवा की। सन् 1936 में उनका देहांत हो गया।
2. प्रमुख रचनाएँ-मुंशी प्रेमचंद ने आरंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया तथा बाद में हिंदी में आए थे। उन्होंने ‘वरदान’, ‘सेवासदन’, ‘रंगभूमि’, ‘कर्मभूमि’, ‘गबन’, ‘निर्मला’, ‘प्रेमाश्रम’, ‘गोदान’ आदि ग्यारह उपन्यासों की रचना की है तथा तीन सौ के लगभग कहानियाँ लिखी हैं जिनमें ‘कफन’, ‘पूस की रात’, ‘दो बैलों की कथा’, ‘पंच परमेश्वर’, ‘बड़े घर की बेटी’, ‘शतरंज के खिलाड़ी’ आदि प्रमुख हैं।
3. कहानी-कला की विशेषताएँ-मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण कहानी-साहित्य ‘मानसरोवर’ के आठ भागों में संकलित है। कहानी-कला की दृष्टि से प्रेमचंद अपने युग के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। उन्होंने अपने कहानी-साहित्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं को विषय बनाकर कहानी को जन-जीवन से जोड़ा है। उनकी कहानी-कला की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
(i) विषय की विभिन्नता-मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है। उन्होंने जीवन के विविध पक्षों पर जमकर कलम चलाई है। उनकी कहानियों के विषय की व्यापकता पर टिप्पणी करते हुए डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है
“प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और शोषित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद-पद पर लांछित, अपमानित और शोषित नारी जाति की महिमा के वे ज़बरदस्त वकील थे, गरीबों और बेकसों के महत्त्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, सुख-दुःख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज का सजीव चित्र देखा जा सकता है।”
(ii) गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव मुंशी प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद स्वयं यह स्वीकार करते हुए लिखते हैं-“मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका उद्देश्य भी यही है कि मज़दूर और काश्तकार सुखी हों। महात्मा गांधी हिंदू-मुसलमानों की एकता चाहते हैं। मैं भी हिंदी और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूँ।” यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियों में गांधीवादी विचारधारा की झलक सर्वत्र देखी जा सकती है। उनके पात्र गांधीवादी आदर्शों पर चलते हैं और उनका समर्थन करते हैं।
(iii) मानव-स्वभाव का विश्लेषण-मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जहाँ अपने पात्रों के बाह्य आकार व रूप-रंग का वर्णन किया है, वहाँ उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन-विश्लेषण किया है। वे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुक्त कहानी को उत्तम मानते थे। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय में उन्होंने लिखा है-“वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है।”
(iv) ग्रामीण-जीवन का चित्रांकन-मुंशी प्रेमचंद ने जितना ग्रामीण-जीवन का वर्णन किया है, उतना वर्णन किसी अन्य कहानीकार ने नहीं किया। उन्होंने कथा-साहित्य को जन-जीवन से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है। उनकी कहानियों में ग्रामीण-जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। उन्होंने अपने कथा-साहित्य में गाँव के गरीब किसानों, मज़दूरों, काश्तकारों, दलितों और पीड़ितों के प्रति विशेष संवेदना दिखाई है।

(v) आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद-मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है, किन्तु उनके समाधान प्रस्तुत करते हुए आदर्श भी प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, इनकी कहानियों में यथार्थ एवं आदर्श का अनुपम सौंदर्य है। इस विषय में प्रेमचंद जी का स्पष्ट मत है कि साहित्यकार को नग्नताओं का पोषक न बनकर मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को भी दिखाने वाला होना चाहिए।
4. भाषा-शैली-मुंशी प्रेमचंद आरंभ में उर्दू भाषा में लिखते थे और बाद में इन्होंने हिंदी भाषा में लिखना आरंभ किया। इसलिए इनकी लेखन-भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयुक्त होना स्वाभाविक है। इनकी कहानियों की भाषा जितनी सरल, स्पष्ट और भावानुकूल है, उतनी ही व्यावहारिक भी है। लोक-प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रसंगानुकूल प्रयोग से इनकी भाषा में गठन एवं रोचकता का समावेश हुआ है। कहीं-कहीं मुहावरों के प्रयोग की झड़ी-सी लग जाती है। सूक्तियों के प्रयोग में तो प्रेमचंद बेजोड़ हैं।
प्रेमचंद की कहानियों में भावानुकूल एवं पात्रानुकूल भाषा का सार्थक प्रयोग किया गया है। सफल संवाद-योजना के कारण उनकी भाषा-शैली में नाटकीयता के गुण का समावेश हुआ है। कहानियों में वर्णन-शैली के साथ-साथ व्यंग्यात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद जी की भाषा-शैली में प्रेरणा देने की शक्ति के साथ-साथ पाठकों को चिंतन के लिए उकसाने की भी पूर्ण क्षमता है। अपनी कहानी-कला की इन्हीं प्रमुख विशेषताओं के कारण प्रेमचंद अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं।
दो बैलों की कथा पाठ-सार/गद्य-परिचय
प्रश्न-
‘दो बैलों की कथा’ शीर्षक पाठ का सार/गद्य-परिचय अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर-
‘दो बैलों की कथा’ प्रेमचंद की एक महत्त्वपूर्ण कहानी है। इसमें उन्होंने कृषक समाज एवं पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती। उसके लिए बार-बार प्रयास करना पड़ता है तथा आपसी भेदभाव त्यागकर एक-जुट होकर संघर्ष भी करना पड़ता है। कहानी का सार इस प्रकार है-
लेखक ने बताया है कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है, क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है। वह किसी बात का विरोध नहीं करता। अन्य जानवरों को कभी-न-कभी गुस्सा आ जाता है, किन्तु गधे को कभी गुस्सा करते नहीं देखा। बैल के विषय में लोगों की कुछ और ही धारणा रही है तभी तो उसे ‘बछिया का ताऊ’ कहते हैं। किन्तु यह बात सच नहीं है क्योंकि बैल को गुस्सा भी आता है, वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपना लेता है। इसलिए उसे लोग गधे से बेहतर समझते हैं।
झूरी काछी के यहाँ दो बैल थे। एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती था। दोनों सुंदर, स्वस्थ और काम करने वाले थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों साथ-साथ रहते और काम करते थे।
संयोगवश एक बार झूरी ने दोनों बैल अपने साले गया को दे दिए। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। अतः गया को बैलों को घर तक ले जाने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। शाम को जब वे गया के घर पहुंचे तो उन्होंने घास को मुँह तक नहीं लगाया। दोनों आपस में मूक भाषा में सलाह कर रात को रस्सियाँ तुड़वाकर झूरी के घर की ओर चल पड़ते हैं। झूरी प्रातःकाल उठकर देखता है कि उसके दोनों बैल नाद पर खड़े घास खा रहे हैं। झूरी दौड़कर स्नेहवश दोनों को गले से लगा लेता है। गाँव के सभी लोग बैलों की स्वामिभक्ति पर आश्चर्यचकित थे, किन्तु झूरी की पत्नी से यह देखते न बना। वह पति और बैलों को भला-बुरा . बताने लगी।
अगले दिन से पत्नी ने मजदूर को बैलों के पास सूखी घास डालने को कहा। मजदूर ने वैसा ही किया। दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को फिर से ले जाकर मोटी-तगड़ी रस्सियों में बाँधकर सूखा भूसा डाल दिया और अपने बैलों को अच्छा चारा दिया।
अगले दिन दोनों को खेत में जोता गया, लेकिन मार खाने पर भी दोनों ने पैर न उठाने की कसम खा रखी थी। अधिक मार खाने पर दोनों भाग खड़े हुए। मोती के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, किन्तु हीरा के समझाने पर मोती खड़ा हो गया। गया ने दूसरे लोगों की सहायता से उसको पकड़ा और घर ले जाकर फिर मोटी रस्सियों में बाँध दिया तथा फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया।
इस प्रकार दोनों बैल दिन-भर परिश्रम करते और मार खाते और संध्या के समय सूखा भूसा खाते। एक दिन गया की लड़की ने दोनों को खोल दिया और फिर शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गाँव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया, लेकिन बैल भाग चुके थे। दोनों बैल भागते-भागते अपनी राह भी भूल बैठे। अब वे भूख से बेहाल थे, लेकिन पास ही मटर का खेत देखकर उसमें चरने लगे और फिर खेलने लगे। कुछ ही देर में उधर एक साँड आया और उनसे भिड़ गया। दोनों ने जान हथेली पर रखकर बड़े प्रयत्न से उसे आगे-पीछे से रौंदना शुरू किया। दोनों ने बड़े साहस के साथ साँड पर विजय प्राप्त की। साँड मार खाकर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर भूख लग गई थी। सामने मटर का खेत देखकर उसमें पुनः चरने लगे थे। किन्तु थोड़ी देर में खेत के रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांजीहौस में बंद कर दिया।
कांजीहौस में उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें रात-भर किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। वे भूख के मारे मरे जा रहे थे। हीरा के मन में विद्रोह भड़क उठा। मोती के समझाने पर भी वह न माना और उसने सामने कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पशुओं को गिनने आया। हीरा को इस प्रकार दीवार तोड़ते देखकर उसने उसको रस्सी से बाँधकर कई डंडे दे मारे। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी साहस बटोरकर दीवार गिरानी आरंभ कर दी। इस प्रकार काफी संघर्ष के बाद आधी दीवार गिर गई। काफी जानवर भाग निकले। मोती ने फिर हीरा की रस्सी काटनी आरंभ की, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। के. दोनों वहीं पड़े रहे।
एक सप्ताह तक वे दोनों कांजीहौस में भूखे मरते रहे। वे बहुत ही कमजोर पड़ गए थे। दोनों बैलों को एक दढ़ियल के हाथों नीलाम कर दिया गया। दढ़ियल उन्हें लिए जा रहा था कि दोनों को परिचित राह मिल गई और वे उससे छूटकर सीधे झूरी के घर जा पहुँचे। झूरी धूप सेक रहा था। बैलों को आता देखकर उसने उन्हें गले से लगा लिया। झूरी और दढ़ियल में झगड़ा हो गया। किन्तु बैलों को फिर वही स्नेह मिला। झूरी ने उनकी पीठ सहलाई और मालकिन ने उनका माथा चूम लिया। दोनों बैलों को अच्छा चारा दिया गया। वे दोनों अब सुखद अनुभव कर रहे थे।
कठिन शब्दों के अर्थ –
(पृष्ठ-5) : ज्यादा = अधिक। बुद्धिहीन = मूर्ख । परले दरजे का बेवकूफ = अत्यधिक मूर्ख । निरापद = सुरक्षित। सहिष्णुता = सहनशीलता। अनायास = अचानक ही। कुलेल करना = खेलकूद करना। विषाद = निराशा, दुःख। पराकाष्ठा = चरम सीमा। अनादर = अपमान। दुर्दशा = बुरी हालत। कुसमय = बुरा समय। जी तोड़कर काम करना = खूब परिश्रम करना। गम खाना = चुप रहना। ईंट का जवाब पत्थर से देना = मुँह तोड़ जवाब देना।
(पृष्ठ-6) : मिसाल = उदाहरण। गण्य = प्रमुख। बछिया का ताऊ = सीधा। अड़ियल = जिद्दी। काछी = किसान। पछाईं = पालतू पशुओं की एक नस्ल। डील = कद। विचार-विनिमय = विचारों का आदान-प्रदान। वंचित = रहित, न मिलना। विग्रह = अलग होना। आत्मीयता = अपनेपन का भाव। घनिष्ठता = समीपता। फुसफुसी = हल्की, दिखावटी। वक्त = समय।
(पृष्ठ-7) : दाँतों पसीना आना = खूब परिश्रम करना। पगहिया = पशु बाँधने की रस्सियाँ। हुँकारना = गुस्से से आवाज निकालना। कोई कसर न उठा रखना = कोई कमी न छोड़ना। चाकरी = सेवा। जालिम = निर्दयी। मूक-भाषा = मौन भाषा। अनुमान होना = अंदाजा लगाना। गराँव = रस्सी जो बैलों के गले में बाँधी जाती है। विद्रोहमय = क्रांतियुक्त। प्रेमालिंगन = प्रेम से गले लगाना। मनोहर = सुंदर। अभूतपूर्व = जो पहले कभी न हुई हो।
(पृष्ठ-8) : प्रतिवाद = विरोध करना। साहस न होना = हौंसला न पड़ना। जल उठना = अत्यधिक गुस्सा आना। नमक हराम = किए हुए उपकार को न मानने वाला। कामचोर = काम न करने वाला। ताकीद करना = आदेश देना।

(पृष्ठ-9) : मजा चखाना = बदला लेना, तंग करना। टिटकार = मुँह से निकलने वाला टिक-टिक का शब्द। आहत = घायल। सम्मान = इज्जत, आदर। व्यथा = पीड़ा। काबू से बाहर होना = सीमा से बाहर होना। व्यर्थ = बेकार।
(पृष्ठ-10) : दिल में ऐंठकर रह जाना = विवश होना। तेवर = गुस्से से युक्त शक्ल। मसलहत = हितकर। सज्जन = भला व्यक्ति।
(पृष्ठ-11) : बरकत = संतुष्टि। दुर्बल = कमजोर। विद्रोह = क्रांति, गुस्सा। अनाथ = जिसका कोई नहीं होता। उपाय = साधन। सहसा = अचानक। गराँव = पशुओं को बाँधने वाली रस्सियाँ । आफत आना = मुसीबत आना। संदेह = शंका।
(पृष्ठ-12) : हड़बड़ाकर = घबराकर । मौका = अवसर। बेतहाशा = बिना सोचे-समझे । व्याकुल = बेचैन। आहट = किसी के आने की ध्वनि। आज़ादी = स्वतंत्रता। बगलें झाँकना = डर के कारण इधर-उधर देखना। आरजू = इच्छा।
(पृष्ठ-13) : कायरता = डरपोकपन। नौ-दो ग्यारह होना = भाग जाना। रगेदना = खदेड़ना। जोखिम = खतरा। हथेलियों पर जान लेना = जीवन को खतरे में डालना। मल्लयुद्ध = कुश्ती। बेदम होना = थक जाना।
(पृष्ठ-14) : संगी = साथी। कांजीहौस = मवेशीखाना, वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है और कुछ दंड लगाकर छोड़ दिया जाता है। साबिका = वास्ता। टकटकी लगाए ताकना = निरंतर देखते रहना। विद्रोह की ज्वाला दहक उठना = क्रांति की भावना जागृत होना। हिम्मत हारना = साहस या धीरज त्यागना।
(पृष्ठ-15) : उजड्डपन = शरारतीपन। डडे रसीद करना = डंडे मारना। जान से हाथ धोना = जीवन गँवाना। प्रतिद्वंद्वी= विरोधी। जोर-आज़माई = शक्ति लगाना।
(पृष्ठ-16) : विपत्ति = मुसीबत। अपराध = दोष, कसूर । खलबली मचना = बेचैनी उत्पन्न होना। मरम्मत होना = मार पड़ना। ठठरियाँ = हड्डियाँ। मृतक = मरा हुआ।
(पृष्ठ-17) : सहसा = अचानक। दढ़ियल = दाढ़ी वाला। अंतर्ज्ञान = आत्मा का ज्ञान। दिल काँप उठना = भयभीत हो जाना। भीत नेत्र = डरी हुई आँखें। नाहक = व्यर्थ में। नीलाम होना = बोली पर बिकना। रेवड़ = पशुओं का समूह। पागुर करना = जुगाली करना। प्रतिक्षण = हर पल । दुर्बलता = कमजोरी। गायब होना = समाप्त होना।
(पृष्ठ-18-19) : उन्मत्त = मतवाले। कुलेलें करना = क्रीड़ा करना । अख्तियार = अधिकार। रास्ता देखना = प्रतीक्षा करना। शूर = बहादुर। उछाह-सा = उत्साह ।
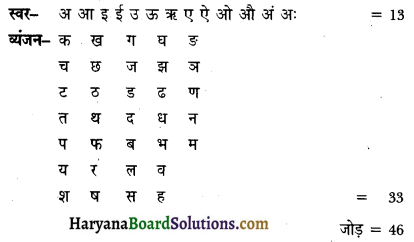
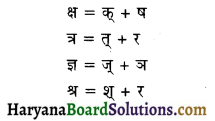
![]()
![]()
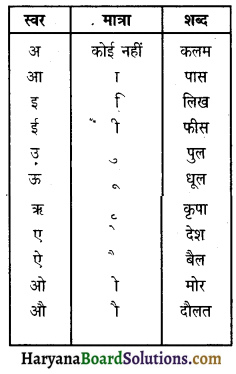
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()