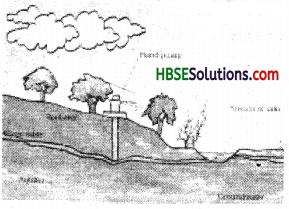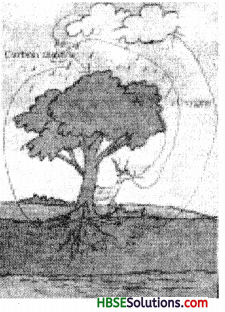HBSE 12th Class Hindi Solutions Vitan Chapter 4 डायरी के पन्ने
Haryana State Board HBSE 12th Class Hindi Solutions Vitan Chapter 4 डायरी के पन्ने Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Hindi Solutions Vitan Chapter 4 डायरी के पन्ने
HBSE 12th Class Hindi डायरी के पन्ने Textbook Questions and Answers
प्रश्न 1.
“यह साठ लाख लोगों की तरफ से बोलनेवाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़, जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की है।” इल्या इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में ऐन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें।
उत्तर:
ऐन फ्रैंक की डायरी में उसके निजी जीवन का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि साठ लाख यहूदियों पर जो अत्याचार किए गए थे उनकी यह जीती-जागती कहानी है। यह लड़की न कोई संत थी, न कवि बल्कि हिटलर के अत्याचारों के द्वारा भूमिगत रहने वाले परिवार की एक आम सदस्या थी। वह कोई विशेष लड़की नहीं थी, परंतु वह एक ऐसी आवाज थी जिसमें अत्याचार सहन करने वाले लोगों की आवाज को बुलंद किया। अतः इल्या इहरनबुर्ग की टिप्पणी पूर्णतया सही है। दूसरे विश्वयुद्ध में हिटलर ने यहूदियों पर अत्यंत अत्याचार किए। यहूदी भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए।
हिटलर की सेना का इतना डर बैठा हुआ था कि यहूदी लोग भूमिगत होकर अभावग्रस्त जीवन जी रहे थे। वे लोग न दिन का सूरज देख सकते थे और न ही रात का चंद्रमा। सड़क पर सूटकेस लेकर निकलना निरापद नहीं था। ब्लैक कोड वाले पर्दे लगाकर जैसे-तैसे दिन और रात व्यतीत करते थे। राशन की बहुत कमी रहती थी और बिजली का कोटा निर्धारित था। चोर-उच्चके उनके सामान को उठा लेते थे। यहूदी लोग फटे-पुराने कपड़े तथा घिसे-पिटे जूते पहनकर समय काट रहे थे। जब कभी हवाई आक्रमण होता था तो बेचारे काँप जाते थे। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित है कि डायरी के पन्ने में वर्णित कहानी किसी एक परिवार की नहीं है बल्कि यह साठ लाख लोगों की कहानी है।
प्रश्न 2.
“काश, कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला…..।” क्या आपको लगता है कि ऐन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है?
उत्तर:
यह एक सच्चाई है कि लेखक अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कविता, कहानी या कोई लेख लिखता है। यदि लिखने वाला व्यक्ति किसी के सामने अपनी बात को प्रकट कर देता है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु यदि उसे कोई गंभीर श्रोता न मिले तो वह किसी कल्पित पात्र अथवा पाठकों के लिए अपनी अभिव्यक्ति करता है। ऐन फ्रैंक के साम यही स्थिति थी। वह भूमिगत रहने वाले सदस्यों में सबसे छोटी थी। कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मिसेज वान दान तथा मिस्टर डसेल उसकी कमियाँ निकालते रहते थे। इसलिए वह उनसे घृणा करती थी।
उसकी मम्मी हमेशा केवल एक उपदेशिका की भूमिका निभाती रही। उसने कभी भी अपनी बेटी की व्यथा नहीं सुनी। केवल पीटर से ही ऐन की बनती थी लेकिन उसके साथ संवाद करना सरल न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भूमिगत आवास में वह क्या करे। वह बाहर की प्रकृति को देखना चाहती थी, सूरज तथा चाँद को निहारना चाहती थी परंतु यह वर्जित था। वह निर्णय नहीं कर पाई कि वह किसके सामने अपनी भावनाएँ प्रकट करें। सच्चाई तो यह है कि उसकी भावनाओं को और उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसने अपने उद्गार इस डायरी में व्यक्त किए हैं।
![]()
प्रश्न 3.
‘प्रकृति-प्रदत्त प्रजनन-शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें इस की स्वतंत्रता स्त्री से छीन कर हमारी विश्व-व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व-विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है।’ ऐन की डायरी के 13 जून, 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूँढ़ें।।
उत्तर:
ऐन का विचार है कि पुरुष शारीरिक दृष्टि से सक्षम होता है और नारियाँ कमज़ोर होती हैं इसलिए पुरुष नारियों पर शासन करते हैं। उसका कहना है कि नारियों को समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता। बच्चे को जन्म देते समय नारी जो पीड़ा व व्यथा भोगती है, वह युद्ध में घायल हुए सैनिक से कम नहीं है। सच्चाई तो यह है कि नारी अपनी बेवकूफी के कारण अपमान व उपेक्षा को सहन करती रहती हैं, परंतु नारियों को समाज में उचित सम्मान मिले यह जरूरी है। परंतु ऐन का यह अभिप्राय नहीं है कि महिलाएँ बच्चा पैदा करने बंद कर दें। प्रकृति चाहती है कि महिलाएँ बच्चों को जन्म दें। समाज में औरतों का योगदान विशेष महत्त्व रखता है। ऐन का यह भी विचार है कि आने वाले काल में औरतों के लिए बच्चे पैदा करना कोई जरूरी नहीं होगा।
अब समय काफी बदल चुका है। हमारा देश परंपरावादी है। इसलिए यहाँ महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। जहाँ तक अशिक्षित ग्रामीण समाज का प्रश्न है वहाँ पर पुरुष स्त्रियों पर हावी रहते हैं। शिक्षित समाज में स्त्रियाँ पुरुषों से बेहतर हैं। उन्हें घर-परिवार, समाज, समूह, राष्ट्र सभी स्थानों पर सम्मान मिल रहा है। अब बच्चा पैदा करना या न करना अब नारी के हाथ में है। इसलिए ऐन फ्रैंक की डायरी में वर्णित नारी की स्थिति की तुलना में भारतीय स्थिति की हालत काफी बेहतर है। हमारे यहाँ नारियाँ सरकारी व गैर-सरकारी विभागों में नौकरियाँ कर रही हैं जिनमें से कुछ नारियाँ डॉक्टर हैं तो कुछ इंजीनियर हैं। शिक्षा जगत में तो नारियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है।
प्रश्न 4.
“ऐन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज़ है, तो साथ ही उसके निजी सुख-दुख और भावनात्मक उथल-पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है।” इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें।
उत्तर:
डायरी लेखक जब अपने जीवन का वर्णन करता है तब वह अपने आसपास के वातावरण पर भी प्रकाश डालता है। ऐन एक सामान्य लड़की है वह कोई साहित्यकार नहीं है। फिर भी उसने अपने निजी सुख-दुख और भावनात्मक उथल-पुथल का संवेदनात्मक वर्णन किया है। जिस परिवेश में वह रहने को मजबूर है वह असाधारण है। जर्मनी ने हॉलैंड पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, परंतु ब्रिटेन हॉलैंड को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ रहा था। दूसरी तरफ यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे। वे भूमिगत होकर अभावमय और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐन भी उन्हीं में से एक है। इसलिए ऐन ने व्यक्तिगत जीवन के सुख-दुख और भावनात्मक उथल-पुथल का संवेदनात्मक वर्णन किया है।
लेकिन ऐन तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है; जैसे अज्ञातवास जाने के कारण का बुलावा, आवास में जर्मनों के डर के कारण दिन-रात अंधकार में छिपकर रहना, युद्ध के अवसर पर राशन तथा बिजली की कमी होना, लड़की द्वारा तटस्थता की घोषणा करना, ब्रिटेन द्वारा हॉलैंड को मुक्त कराने का प्रयास करना, प्रतिदिन 350 वायुयानों द्वारा 550 टन गोले बारूद की वर्षा करना, हिटलर के सैनिकों द्वारा दिए गए साक्षात्कार का रेडियो पर विवरण आदि तत्कालीन ऐतिहासिक दौर के जीवंत दस्तावेज कहे जा सकते हैं। ऐन ने निजी जीवन की व्यथा के साथ-साथ इन ऐतिहासिक तथ्यों का यदा-कदा वर्णन किया है जिससे दोनों का अंतर मिट गया है।
![]()
प्रश्न 5.
ऐन ने अपनी डायरी ‘किट्टी’ (एक निर्जीव गुड़िया) को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी?
उत्तर:
आठ सदस्य अज्ञातवास में रह रहे थे। इनमें ऐन सबसे छोटी आयु की लड़की थी। इस आयु की लड़कियाँ किसी से बात करना चाहती हैं। परंतु आठ सदस्यों में से कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। भूमिगत आवास में से बाहर निकलना संभव नहीं है। उसकी माँ केवल उपदेश देती है। मिसेज वान दान और मिस्टर डसेल उसकी हर बात की नुक्ता-चीनी करती रहती थीं। सात सदस्यों की बातें वही हजारों बार सुन चुकी है। इसलिए वह अपनी गुड़िया किट्टी से बातचीत करती है। यही बातचीत उसके डायरी के पन्ने बन गए हैं। इसमें वे पत्र भी हैं जो उसने अपनी गुड़िया किट्टी को लिखे थे। किट्टी को संबोधित करके चिट्ठियाँ लिखना उसकी मजबूरी थी।
इसे भी जानें
नाजी दस्तावेजों के पाँच करोड़ पन्नों में ऐन फ्रैंक का नाम केवल एक बार आया है लेकिन अपने लेखन के कारण आज ऐन हज़ारों पन्नों में दर्ज हैं जिसका एक नमूना यह खबर भी है
उत्तर:
नाज़ी अभिलेखागार के दस्तावेजों में महज़ एक नाम के रूप में दफन है ऐन फ्रैंक बादरोलसेन, 26 नवंबर (एपी)। नाज़ी यातना शिविरों का रोंगटे खड़े करने वाला चित्रण कर दुनिया भर में मशहूर हुई ऐनी फ्रैंक का नाम हॉलैंड के उन हज़ारों लोगों की सूची में महज़ एक नाम के रूप में दर्ज है जो यातना शिविरों में बंद थे।
नाज़ी नरसंहार से जुड़े दस्तावेज़ों के दुनिया के सबसे बड़े अभिलेखागार एक जीर्ण-शीर्ण फाइल में 40 नंबर के आगे लिखा हुआ है-ऐनी फ्रैंक। ऐनी की डायरी ने उसे विश्व में खास बना लिया लेकिन 1944 में सितंबर माह के किसी एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह एक नाम भर थी। एक भयभीत बच्ची जिसे बाकी 1018 यहूदियों के साथ पशुओं को ढोने वाली गाड़ी में पूर्व में स्थित एक यातना शिविर के लिए रवाना कर दिया गया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डच रेडक्रास ने वेस्टरबोर्क ट्रांजिट कैंप से यातना शिविरों में भेजे गए लोगों संबंधी सूचना एकत्र कर इंटरनेशनल ट्रेसिंग सर्विस (आईटीएस) को भेजे थे। आईटीएस नाज़ी दस्तावेजों का एक ऐसा अभिलेखागार है जिसकी स्थापना युद्ध के बाद लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए की गई थी।
इस युद्ध के समाप्त होने के छह दशक से अधिक समय के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति विशाल आईटीएस अभिलेखागार को युद्ध में जिंदा बचे लोगों, उनके रिश्तेदारों व शोधकर्ताओं के लिए पहली बार सार्वजनिक करने जा रही है। एक करोड़ 75 लाख लोगों के बारे में दर्ज इस रिकार्ड का इस्तेमाल अभी तक परिजनों को मिलाने, लाखों विस्थापित लोगों के भविष्य का पता लगाने और बाद में मुआवजे के दावों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने में किया जाता रहा है। लेकिन आम लोगों को इसे देखने की अनुमति नहीं दी गई है।
मध्य जर्मनी के इस शहर में 25.7 किलोमीटर लंबी अलमारियों और कैबिनेटों में संग्रहीत इन फाइलों में उन हज़ारों यातना शिविरों, बंधुआ मजदूर केंद्रों और उत्पीड़न केंद्रों से जुड़े दस्तावेजों का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है।
किसी ज़माने में थर्ड रीख के रूप में प्रसिद्ध इस शहर में कई अभिलेखागार हैं। प्रत्येक में युद्ध से जुड़ी त्रासदियों का लेखा-जोखा रखा गया है। आईटीएस में एनी फ्रैंक का नाम नाज़ी दस्तावेजों के पाँच करोड़ पन्नों में केवल एक बार आया है। वेस्टरबोर्क से 19 मई से 6 सितंबर 1944 के बीच भेजे गए लोगों से जुड़ी फाइल में फ्रैंक उपनाम से दर्जनों नाम दर्ज हैं।
में ऐनी का नाम, जन्मतिथि. एम्सटर्डम का पता और यातना शिविर के लिए रवाना होने की तारीख दर्ज है। इन लोगों को कहाँ ले जाया गया वह कालम खाली छोड़ दिया गया है। आईटीएस के प्रमुख यूडो जोस्त ने पोलैंड के यातना शिविर का जिक्र करते हुए कहा यदि स्थान का नाम नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यह आशविच था। ऐनी, उनकी बहन मार्गोट व उसके माता-पिता को चार अन्य यहूदियों के साथ 1944 में गिरफ्तार किया गया था। ऐनी डच नागरिक नहीं जर्मन शरणार्थी थी। यातना शिविरों के बारे में ऐनी की डायरी 1952 में ‘ऐनी फ्रैंक दी डायरी ऑफ़ द यंग गर्ल’ शीर्षक से छपी थी।
-साभार जनसत्ता 27 नवंबर, 2006
HBSE 12th Class Hindi डायरी के पन्ने Important Questions and Answers
प्रश्न 1.
‘डायरी के पन्ने’ नामक पाठ के आधार पर सेंधमारों वाली घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
उत्तर:
युद्ध काल में सेंधमारों ने आम जीवन को कष्टमय बना दिया था। बेचारे डॉक्टर अपने मरीजों को देख नहीं पाते थे। जैसे ही वे अपनी पीठ मोड़ते थे, उनकी कारें व मोटर साइकिलें चुरा ली जाती थीं। चोरी-चकारी निरंतर बढ़ती जा रही थी। डच लोगों ने हाथों में अंगूठी पहनना बंद कर दिया था। आठ-दस साल के छोटे बच्चे भी खिड़कियाँ तोड़कर घरों में घुस जाते थे और जो कुछ मिलता था, उसे उठाकर ले जाते थे। कोई भी आदमी पाँच मिनट के लिए अपना घर खाली नहीं छोड़ सकता था। टाइपराइटर, ईरानी कालीन, बिजली से चलने वाली घड़ियाँ, कपड़े आदि चोरी हो जाते थे। उन्हें वापिस पाने के लिए लोग अपने विज्ञापन देते रहते थे। सेंधमार गली व नुक्कड़ों पर लगी हुई बिजली से चलने वाली घड़ियाँ उतार लेते थे और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा-पुर्जा अलग कर देते थे। मालिकों के उठने तक वे भाग जाते थे। उसके हटते ही पुनः आ जाते थे। गोदाम में जब वे सेंधमारी कर रहे थे, तब पुलिस की आवाज़ सुनकर भाग गए। पर फाटक बंद करते ही वे पुनः वापस आ गए। जब दरवाजे पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, तब सेंधमार भाग गए।
प्रश्न 2.
हजार गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित करने से उत्पन्न कठिनाइयों का विवेचन कीजिए।
उत्तर:
हजार गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने के पीछे ब्लैक मार्किट का काम करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए एक भारी झटका तो था, किन्तु जन-साधारण के लिए तो एक बड़ा संकट भी था। क्योंकि जो लोग भूमिगत थे या जो अपने धन का हिसाब-किताब नहीं दे सकते ये उनके लिए भी संकट का समय था। हजार गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हों कि यह नोट आपके पास आया कैसे और इसका सबूत भी देना पड़ता था। इन्हें कर अदा करने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। वह भी केवल एक सप्ताह तक ही। इस प्रकार हजार गिल्डर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित करने से भूमिगत लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी।
![]()
प्रश्न 3.
अपने मददगारों के बारे में ऐन ने क्या लिखा है?
उत्तर:
अपने मददगारों के बारे में ऐन ने लिखा है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। ऐन आशावान है कि ये उन्हें सुरक्षित बचा लेंगे। उनके बारे में वे लिखती भी हैं, “उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं। हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें यह बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं।”
प्रश्न 4.
‘डायरी के पन्ने पढ़कर आपके मन पर कैसी प्रतिक्रिया होती है?
उत्तर:
‘डायरी के पन्ने’ ऐन फ्रैंक की एक सफल डायरी कही जा सकती है। यद्यपि ऐन फ्रैंक कोई साहित्यकार नहीं थी लेकिन जिस प्रकार उसने विश्वयुद्ध के काल में जर्मनी द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है, वह यथार्थपरक बन पड़ा है। हिटलर सचमुच एक क्रूर शासक था। वह यहूदियों से अत्यधिक घृणा करता था। उसने लाखों नागरिकों को यातनाएँ देकर मार डाला। इस डायरी को पढ़कर हमारे मन पर यह प्रतिक्रिया होती है कि युद्ध और कट्टर जातिवाद दोनों ही भयानक हैं। जातीय अहंकार का शिकार बना हुआ शासक हिंसक पशु बन जाता है और वह अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। यही कुछ हिटलर और उसके सैनिकों ने किया। डायरी पढ़ने से हमारे मन में उन लोगों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है जो बेकसूर होते हुए भी अत्याचारों के शिकार बनें। उन्हें छिपकर रहना पड़ा और लंबे काल तक सर्य चंद्रमा, खली हवा, धूप आदि से वंचित रहना पड़ा। यह डायरी हमारे मन में करुणा की भावनाएँ जगाती है और पाठकों को यह संदेश देती है कि अत्याचारी शासकों का डटकर विरोध करना चाहिए।
प्रश्न 5.
मिसेज बान दान की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर:
मिसेज बान दान ऐन के परिवार की मित्र महिला है। इसके पति और ऐन के पिता में मित्रता थी। इनका परिवार भी ऐन के परिवार के साथ अज्ञातवास में रहता है। मिसेज बान दान ऐन के परिवार के लिए बहुत-सी जरूरत की वस्तुएँ लाकर देती है। कहने का तात्पर्य है कि मिसेज बान दान दूसरों की कठिनई एवं दुःख-दर्द भली-भाँति अनुभव ही नहीं करती, अपितु उनकी सहायता भी करती है। इससे पता चलता है कि मिसेज बान-दान एक भली, दयावान और सहयोगी नारी है।
प्रश्न 6.
लेखिका के पिता किस कारण से नर्वस हो गए थे?
उत्तर:
लेखिका के पिता एक दिन बहुत-ही घबराए हुए थे। एक रात उनके घर के नीचे वाले गोदाम में चोरी और लूट-मार करने के लिए कुछ सेंधमार घुस गए। उन्होंने गोदाम के दरवाजे का फट्टा गिरा दिया और लूट-माट करने लगे। लेखिका के पिता और वान दान परिवार ऊपर छिपकर रह रहे थे। वे चोरों के सामने नहीं आना चाहते थे, तब अचानक वान दान पुलिस कहकर चिल्लाया। पुलिस शब्द सुनते ही सेंधमार भाग गए। अगले ही क्षण फट्टा फिर गिरा दिया गया और सेंधमार फिर से चोरी करने लगे। यह सब देखकर लेखिका का पिता घबरा गया। उसे डर था कि यदि पुलिस आ गई तो उन्हें हिटलर के यातना शिविरों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे नर्वस हो गए थे।
![]()
प्रश्न 7.
मिस्टर डसेल के चरित्र पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
मिस्टर डसेल एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह बड़ा सनकी, झक्की, ऊबाने वाला और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। वह पुराने जमाने के अनुशासन में विश्वास करता था और बात-बात पर लंबे भाषण देने लगता था। यदि कोई व्यक्ति उनके कहे अनुसार काम नहीं करता था तो वह उन्हें फटकारने लगता था। उनके चरित्र की बड़ी कमज़ोरी यह थी कि वह चुगलखोर था। वह अकसर लेखिका की चुगली उसकी माँ से कर देता था। फिर ऐन को माँ के लंबे उपदेश सुनने पड़ते थे। वह बड़ा ही क्रोधी और असहनशील व्यक्ति भी था। एक बार जब किसी ने उसका कुशन उठा लिया तो वह बहुत-ही व्याकुल और बेचैन हो उठा। सारा घर सिर पर उठा लिया।
प्रश्न 8.
ऐन फ्रैंक के फिल्मी प्रेम पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
ऐन फ्रैंक तेरह-चौदह वर्ष की किशोरी थी। इस आयु में फिल्मों व फिल्मी कलाकारों के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। किन्तु ऐन फ्रैंक ऐसी नहीं थी, अपितु वह बहुत गम्भीर स्वभाव वाली थी। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती थी। यद्यपि उसके परिवार वाले फिल्मी सिनेमा की पत्रिका आदि को पैसों की बरबादी मानते थे। उसे फिल्म व फिल्मी कलाकारों के प्रति इतना प्रेम था कि वह एक वर्ष बाद भी किसी फिल्म के से सकती थी। जब बेप उसे बताती थी कि शनिवार को वह फलां फिल्म देखने जाना चाहती है तो वह उस फिल्म के मुख्य नायक-नायिकाओं के नाम एवं समीक्षा फर्राटे से बता देती थी। उसकी माँ ने तो व्यंग्य में यहाँ तक कह डाला इसे फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐन को सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएँ ज़बानी याद हैं। अतः इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐन फ्रैंक को फिल्मों के प्रति अत्यधिक प्रेम था।
प्रश्न 9.
ऐसी कौन-सी घटना हुई जिससे ऐन को लगा कि उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट गई है?
उत्तर:
8 जुलाई, 1942 को ऐन फ्रैंक के परिवार को यह संदेश मिला कि ऐन की बहन मार्गोट का ए०एस०एस० से बुलावा आया था। इसका मतलब था उसे यातना शिविर में भेजना और उसे जर्मन सेना के हवाले करना। यह समाचार पाकर ऐन अत्यधिक घबरा गई थी। उसके माता-पिता किसी भी शर्त पर मार्गोट को यातना शिविर पर नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तत्काल भूमिगत होने का फैसला कर लिया। इस घटना से ऐन को ऐसा लगा कि जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई हो।
प्रश्न 10.
‘डायरी के पन्न’ नामक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए एन बहुत ही प्रतिभाशाली तथा परिपक्व युवती थी।
अथवा
‘डायरी के पन्ने के आधार पर ऐन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
‘डायरी के पन्ने’ से हमें पता चलता है कि ऐन एक प्रतिभावान और धैर्यवान युवती थी। उसमें सहजता और शालीनता थी। किशोरावस्था की चंचलता उसमें बहुत कम दिखाई देती थी। वह बहुत कम अवसरों पर विचलित और बेचैन होती थी। उसने अपने स्वभाव पर नियंत्रण पा लिया था। उसकी सोच सकारात्मक, परिपक्व और सुलझी हुई थी। उसमें अत्यधिक सहनशीलता और संवेदनशीलता थी। वह बड़ों की गलत बातों को भी बड़ी शालीनता से सुनती थी और उनके प्रति सम्मान की भावना रखती थी। पीटर के प्रति भले ही उसके मन में प्रेम हो परंतु वह अपनी भावनाओं को डायरी में ही लिखती थी। किशोरावस्था। सराहनीय है। अपनी परिपक्व सोच के कारण ही उसने अपने मन के भाव और उद्गार डायरी में व्यक्त किए। यदि उसके चरित्र में धैर्य, शालीनता और परिपक्वता न होती तो शायद हमें इतनी उत्कृष्ट डायरी पढ़ने को न मिलती।
प्रश्न 11.
ऐन के स्त्री-पुरुष अधिकारों पर क्या विचार थे?
उत्तर:
ऐन का विचार है कि पुरुष शारीरिक दृष्टि से सक्षम होता है और नारियाँ कमज़ोर होती हैं इसलिए पुरुष नारियों पर शासन करते हैं। उसका कहना है कि नारियों को समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता। बच्चे को जन्म देते समय नारी जो पीड़ा व व्यथा भोगती है, वह युद्ध में घायल हुए सैनिक से कम नहीं है। सच्चाई तो यह है कि नारियाँ अपनी बेवकूफी के कारण अपमान व उपेक्षा को सहन करती रहती हैं, परन्तु नारियों को समाज में उचित सम्मान मिले यह जरूरी है। परंतु ऐन का यह अभिप्राय नहीं है कि महिलाएँ बच्चे पैदा करने बंद कर दें। प्रकृति चाहती है कि महिलाएँ बच्चों को जन्म दें। समाज में औरतों का योगदान विशेष महत्त्व रखता है। ऐन का यह भी विचार है कि आने वाले काल में औरतों के लिए बच्चे पैदा करना कोई जरूरी नहीं होगा।
अब समय काफी बदल चुका है। अब महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। शिक्षित समाज में स्त्रियाँ पुरुषों से बेहतर हैं। उन्हें घर-परिवार, समाज, समूह, राष्ट्र सभी स्थानों पर सम्मान मिल रहा है। बच्चा पैदा करना या न करना अब नारी के हाथ में है। इसलिए ऐन फ्रैंक की डायरी में वर्णित नारी की स्थिति की तुलना में भारतीय नारी की हालत काफी बेहतर है। हमारे यहाँ नारियाँ सरकारी व गैर-सरकारी विभागों में नौकरियाँ कर रही हैं जिनमें से कुछ नारियाँ डॉक्टर हैं तो कुछ इंजीनियर हैं। शिक्षा जगत में तो नारियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है।
प्रश्न 12.
हिटलर अपने सैनिकों से मुख्य रूप से क्या पूछा करता था?
उत्तर:
हिटलर और उसके सैनिकों की बात को अकसर रेडियो पर प्रसारित किया जाता था। बातों का मुख्य विषय युद्ध में घायल हुए सैनिकों का हाल-चाल जानना होता था। हिटलर अपने घायल सैनिकों का हाल-चाल जानकर उनका उत्साह बढ़ाते थे। वे अकसर घायल सैनिकों के युद्ध-स्थान का नाम और उनके घायल होने के कारण के बारे में पूछते थे। घायल सैनिक उत्साहपूर्वक अपना नाम, घायल होने का स्थान तथा घायल होने के कारण भी बताते थे। वे बड़े गर्व के साथ अपनी वीरता का बखान करते थे।
प्रश्न 13.
ऐन की अज्ञातवास के समय क्या रुचियाँ थीं?
उत्तर:
अज्ञातवास के समय ऐन अपने-आपको व्यस्त रखने के लिए दूसरों से बातें करती रहती थी। वह उस समय के क्रूर शासन की गतिविधियों में भी रुचि रखती थी। आर्थिक संकट के विषय में सोचकर ऐन चिंतित हो जाती थी। ऐन की रेडियो सुनने में भी रुचि थी। वह तत्कालीन क्रूर शासक हिटलर की गतिविधियों में भी रुचि रखती थी तथा उस समय चल रहे युद्ध में भी ऐन रुचि रखती थी। जो लोग अज्ञातवास में उनकी सहायता कर रहे थे ऐन उनके प्रति दिल से शुक्रिया का भाव रखती थी। वह अपने साथी पीटर से बातचीत करने में भी रुचि रखती थी। ऐन युद्ध के समय तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी रुचि रखती थी। अज्ञातवास के समय महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के प्रति भी विरोध जताती है।
![]()
प्रश्न 14.
ऐन ने अपने थैले में क्या-क्या भरा और क्यों?
उत्तर:
ऐन ने अपने थैले में एक डायरी, कर्लर, रूमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्टियाँ आदि भर ली थीं। क्योंकि जहाँ वह जा रही थी, वहाँ से वस्तुएँ नहीं मिल सकती थीं।
प्रश्न 15.
ऐन फ्रैंक के नारी सम्बद्ध विचारों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
ऐन फ्रैंक भले ही आयु में कम थी, किन्तु उसकी सामाजिक सोच बहुत गम्भीर थी। उसने तत्कालीन नारी समाज की वस्तु स्थिति की ओर भी संकेत किए हैं। वह नारी की स्वतन्त्रता के पक्ष में थी। ऐन को यह बात पंसद नहीं है कि पुरुष कमा कर लाता है और परिवार का पालन-पोषण करता है। इस आधार पर वह नारियों पर रौब जमाता रहे। अब हालात ब अब तक पुरुष की ज्यादतियों को सहती चली आ रही थीं। सौभाग्य से अब शिक्षा तथा प्रगति ने औरतों की आँखें खोल दी हैं। कुछ पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लम्बे अरसे तक इस तरह की स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएँ पूरी तरह स्वतन्त्र होने का हक चाहती हैं।
प्रश्न 16.
कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने क्या घोषित किया था कि जिससे ऐन को खुशी मिली थी?
उत्तर:
कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन में एक उच्च प्रसारण में घोषणा की थी कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पत्रों का संग्रह किया जाएगा। ऐन ने कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊँगी तो लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में रहते हुए हम लोगों के बारे में जानने की लोगों में उत्सुकता होगी।
प्रश्न 17.
जॉन और मिस्टर क्लीमेन के व्यवहार का परिचय दीजिए।
उत्तर:
जॉन और मिस्टर क्लीमेन ऐन के पिता के कार्यालय में काम करते थे। उन दोनों का व्यवहार बहुत ही सहज, सरल, और मानवीय था। वे दूसरों के दुःख-दर्द को अनुभव कर यथासम्भव सहायता व सहयोग करने वाले लोग थे। जब सब लोग अज्ञातवास में थे, उस समय भी उन्होंने ऐन के परिवार की सहायता की थी।
डायरी के पन्ने Summary in Hindi
डायरी के पन्ने लेखक-परिचय
प्रश्न-
ऐन फ्रैंक का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
अथवा
ऐन फ्रैंक का साहित्यिक परिचय दीजिए।
उत्तर:
जीवन-परिचय-ऐन फ्रैंक का जन्म 12 जून, 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नगर में हुआ। उसकी मृत्यु नाज़ियों के यातनागृह में सन् 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हुई। अज्ञातवास काल में ही ऐन फ्रैंक ने अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी लिखी थी। यह डायरी संसार की सर्वाधिक पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः इसका प्रकाशन सन् 1947 में डच भाषा में हुआ। सन् 1952 में यह डायरी ‘दी डायरी ऑफ़ द यंग गर्ल’ के नाम से अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई। तब से ले संपादित, असंपादित तथा आलोचनात्मक अनेक रूपों में प्रकाशित हो चुकी है। यह संसार की बहुचर्चित तथा बहुपठित डायरी मानी गई है जिसमें एक किशोर युवती की संवेदनशील भावनाओं का यथार्थ वर्णन किया गया है। इस पर फिल्म, नाटक तथा धारावाहिक भी बन चुके हैं।
डायरी के पन्ने पाठ का सार
प्रश्न-
ऐन फ्रैंक द्वारा रचित ‘डायरी के पन्ने’ नामक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर:
द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के शासकों के अत्याचारों के फलस्वरूप हॉलैंड के यहूदी परिवारों को असंख्य यातनाओं तथा पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। यहूदियों ने गुप्त तहखानों में छिपकर अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया। उन्हें शारीरिक तथा मानसिक यातनाएँ सहन करनी पड़ी। उन्होंने भूख, गरीबी और बीमारी को झेला। सरकार ने उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। जर्मनी के शासकों ने गैस चैंबरों तथा फायरिंग स्कॉवओडों द्वारा लाखों यहूदियों को मृत्यु की नींद में सुला दिया। ऐसे काल में दो यहूदी परिवार ऐसे भी थे, जिन्होंने एक गुप्त आवास में दो वर्ष तक छिपकर जीवन व्यतीत किया। पहला, ऐन फ्रैंक का परिवार था, जिसमें माता-पिता के अतिरिक्त तेरह वर्षीय ऐन तथा सोलह वर्षीय उसकी बड़ी बहन मार्गोट थी। दूसरा परिवार वान दान दंपति का था। उनका सोलह साल का लड़का भी उनके साथ था। आठवाँ व्यक्ति मिस्टर डसेल था। फ्रैंक के ऑफिस में काम करने वा ईसाई कर्मचारियों ने उनकी खूब सहायता की।
ऐन फ्रैंक ने गुप्त आवास में जो दो वर्ष व्यतीत किए थे, उसकी जीवन-चर्या को डायरी में लिपिबद्ध किया। किंतु 4 अगस्त, 1944 को किसी ने आठों व्यक्तियों के बारे में सरकार को सूचित कर दिया और वे पकड़े गए। परंतु यह डायरी पुलिस के हाथों नहीं लगी। सन् 1945 में ऐन अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। बाद में उसके पिता ओरो फ्रैंक ने सन् 1948 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया। डायरी में ऐन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए चिट्ठियाँ लिखी हैं। इसमें 13 वर्षीय ऐन फ्रैंक ने गुप्त आवासकाल के भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएँ, घृणा, हवाई हमले का भय, अकेलेपन की व्यथा, मानसिक और शारीरिक जरूरतों का यथार्थ वर्णन किया है। वस्तुतः यह डायरी यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीवंत दस्तावेज कही जा सकती है। ‘डायरी के पन्ने’ का सार इस प्रकार है
![]()
बुधवार, 8 जुलाई, 1942-मेरी प्यारी किट्टी, रविवार से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, उसे तुम नहीं जानती। भले ही मैं जीवित हूँ, परंतु मेरी परिस्थितियों के बारे में कुछ मत पूछो। रविवार की दोपहर को मैं तीन बजे के लगभग बाल्कनी में धूप में अलसाई सी बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसी समय मार्गोट ने धीमी आवाज से कहा कि पापा को ए०एस०एस०द्वारा बुलाए जाने का नोटिस मिला है, परंतु माँ पापा के बिजनेस पार्टनर तथा प्रिय मित्र वान दान को मिलने जा चुकी है। बुलावे का समाचार पाकर मैं हक्की-बक्की रह गई। इसका मतलब है यातना शिविर में नारकीय जीवन भोगना। माँ वान दान से यह पूछने गई थी कि कल ही दोनों परिवार छिपने वाले स्थान पर चले जाएँ। उधर पापा यहूदी अस्पताल में किसी मरीज को देखने गए हैं। उसी समय वान दान और माँ घर में आए और उन्होंने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया। मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे। उस समय माँ और वान दान अकेले में वार्तालाप करना चाहते थे। इसलिए उनके कमरे में किसी और को नहीं जाने दिया।
तब मार्गोट ने कहा कि बुलावा पापा के लिए नहीं आया, बल्कि स्वयं उसके लिए आया है। यह सुनकर मैं चीख उठी। उस समय मेरी बहन की उम्र सोलह वर्ष की थी। मेरे मन में यह शंका थी कि हम कहाँ जाकर छिपेंगे। हम दोनों बहनों ने शीघ्र ही आवश्यक सामान थैले में डालना शुरू कर दिया। मैंने एक डायरी, कर्लर, रूमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में रख ली थीं। बाद में हमने मिस्टर क्लिीमेन को फोन करके सांयकाल को अपने घर पर बुलाया। उधर मिस्टर वान मिएप को लेने चले गए। मिएप आ तो गई लेकिन वह रात को पुनः आने का वचन देकर चली गई। रात को वे दोनों सामान से भरा थैला लेकर आ गए। हम सभी इतने डरे हुए थे कि किसी ने खाना तक नहीं खाया। मिएप और जॉन गिएज रात के ग्यारह बजे पहुँचे। ये दोनों पति-पत्नी पापा के अच्छे मित्र थे। रात मुझे गहरी नींद आ गई। हम सबने अपने-अपने शरीर पर बहुत कपड़े पहने, क्योंकि कोई भी यहूदी सूटकेस लेकर नहीं आ सकता था। मिएप ने अपने थैले में स्कूली किताबें भर ली और अज्ञात स्थान के लिए चली गई। साढ़े सात बजे हम भी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े।
तुम्हारी ऐन गुरुवार, 9 जुलाई, 1942-प्यारी किट्टी, मैं और मम्मी-पापा थैले तथा शॉपिंग बैग लेकर तेज बारिश में भीगते हुए घर से निकल पड़े थे। सुबह-सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें ध्यान से देख रहे थे। जब हम गली में प्रवेश कर गए तब मैंने मम्मी-पापा को बातें करते सुना कि हम सबको 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाना होगा, परंतु अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ गया है। इसलिए हमें कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। पापा के ऑफिस की इमारत में ही छिपने का स्थान बनाया गया था। इस इमारत के भू-तल में एक गोदाम था, जहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची की पिसाई होती थी। इस ऑफिस में बेप, मिएप, मिस्टर क्लीमेन काम करते थे। छोटे-से गलियारे में एक छोटा-सा बैंक ऑफिस था, जहाँ दम घोटने वाला अंधकार था, वहाँ मिस्टर कुगलर और वान दान बैठते थे। इस ऑफिस से बाहर निकलकर बंद गलियारे में चार सीढ़ियाँ चढ़कर एक ऑफिस बनाया गया था। जहाँ फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप आदि सब कुछ था। ये सभी उत्तम दरजे की वस्तुएँ थीं। रसोईघर में दो हीटर तथा चूल्हे भी थे। पास ही एक शौचालय था। निचले गलियारे की सीढ़ियों के पास दूसरी मंजिल का रास्ता था। सीढ़ियों के ऊपर हमारी गुप्त एनेक्सी थी। उसके ऊपर फ्रैंक परिवार का कमरा था। एक छोटा-सा कमरा हम दोनों बहनों के लिए बना था।
ऊपर गुसलखाना, शौचालय, एक बिना खिड़कियों वाला कमरा था जिसमें एक वॉस बेसिन भी लगा हुआ था। ऊपर के एक कमरे में वान दान तथा उसकी पत्नी थी, जिसमें एक गैस चूल्हा तथा सिंक भी थी। तुम्हारी ऐन शुक्रवार, 10 जुलाई, 1942-मेरी प्यारी किट्टी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ पर आ गए हैं। मिएप हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर ले गई और फिर वह हमें एनेक्सी में ले गई। मार्गोट वहाँ पहले से ही थी। हमारी बैठक तथा दूसरे कमरे सामान से भरे पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से लेकर छत तक कपड़ों से भरा पड़ा था। मैं और पापा सफाई करने लगे। माँ और मार्गोट थककर गद्दियों पर ही सो गईं। हम दिन-भर काम करते रहे। जब हम थक गए तो हम भी साफ बिस्तरों पर सो गए। अगले दिन हमने अधूरे काम को पूरा किया। बेप और मिएप हमारे राशन कुपन लेकर सामान लेने गए। इधर पापा ने ब्लैक कोड वाले पर्दे लगा दिए। बुधवार तक मैं इस घर की सफाई करने में लगी रही।
तुम्हारी ऐन शनिवार, 28 नवंबर, 1942-मेरी प्यारी किट्टी, इन दिनों हमारे घर में बिजली बहुत खर्च हो रही है। इसलिए अब हमें थोड़ी किफायत करनी होगी। साढ़े चार बजे अँधेरा हो जाता है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। अनेक प्रकार की हरकतें करके हम समय काटते हैं। दिन में हम पर्दे को एक इंच भी नहीं हटा सकते थे। अंधकार हो जाने के बाद हम पर्दे हटाकर पड़ोसियों के घरों की ताका-झाँकी कर लेते हैं। मैं मिस्टर डसेल के साथ एक कमरे में रहती हूँ, जो एक अनुशासन-प्रिय व्यक्ति है, परंतु वह चुगलखोर भी है। वह अकसर मेरी मम्मी से शिकायत कर देता है जिससे मुझे मम्मी का उपदेश सुनना पड़ता है, जिससे पाँच मिनट बाद मम्मी मुझे अपने पास बुला लेती है। यदि परिवार वाले घर के किसी सदस्य को दुत्कारते तथा फटकारते रहें तो उन्हें सहन करना कठिन हो जाता है और मैं दिन-भर अपने कामों के बारे में सोचती हूँ। तब मैं हँसती भी हूँ और रोती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने-आपको बदलूँ। अब मैं और नहीं लिख सकती क्योंकि कागज खत्म हो गया है।
शुक्रवार, 19 मार्च, 1943-मेरी प्यारी किट्टी, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि टर्की इंग्लैंड के साथ मिल गया है, परंतु दुख का समाचार यह है कि हजार गिल्डर का नोट अवैध मुद्रा घोषित किया जा चुका है। अगले हफ्ते तक पाँच सौ गिल्डर के नोट भी अवैध घोषित हो,जाएँगे। इन नोटों को बदलने के लिए जरूरी है कि उनका प्रमाण दिया जाए। जो लोग ब्लैक मार्किट का धंधा करते हैं, उनके लिए तो यह मुसीबत बन गई है क्योंकि उन लोगों के पास अपने धन का कोई हिसाब-किताब नहीं है। गिएज एंड कंपनी के पास जो हजार गिल्डर के नोट थे, वे अगली अदायगी में खर्च किए जा चुके थे। इसलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है। हमने
वितान (भाग 2) (डायरी के पन्ने]
रेडियो पर घायल हिटलर और उसके साथियों की बातें सुनीं जो अपने घावों की चर्चा कर रहे थे। वे अपने जख्म दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उनमें से एक हिटलर से हाथ मिलाने को इतना उत्साहित हो रहा था कि बोल भी नहीं पाया। मिसेज डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया, जिससे वह पूरा साबुन ही नष्ट हो गया। उन्हें प्रति माह घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती थी। मैंने अपने पापा से कहा कि उस साबुन की भुगताई कर दें।
तुम्हारी ऐन शुक्रवार, 23 जनवरी, 1944 मेरी प्यारी किट्टी, मुझे कुछ सप्ताहों से अपने परिवार के वंशजों और राजसी परिवारों के वंशजों की तालिकाओं में गहरी रुचि हो गई। मैं खोज करके अधिक-से-अधिक जानकारी हासिल करना चाहती थी। साथ ही मैं स्कूल का काम भी नियमित रूप से करती थी और रेडियो पर बी०बी०सी० की होम सर्विस को समझती थी।
रविवार को खाली बैठे मैं अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें इकट्ठी करती थी और सोमवार को मिस्टर कुगलर जो पत्रिका देते थे उसे पढ़ती और देखती थी। परिवार के सभी सदस्य समझते थे कि मैं इन पत्र-पत्रिकाओं पर पैसा खराब कर रही हूँ। छुट्टी के दिन बेप अकसर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती, लेकिन मैं पहले से ही उनको उस फिल्म के बारे में सब कुछ बता देती। इस पर मम्मी कहती कि इसे तो फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं नई केश-सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ तो घरवाले मुझे अवश्य ही टोकते हैं कि मैं फलाँ फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा जवाब होता है कि यह स्टाइल मेरा अपना बनाया हुआ है। जब मैं सबकी बातें सुन-सुनकर बोर हो जाती हूँ तो गुसलखाने में जाकर अपने बाल फिर से खोल लेती हूँ। इससे मेरे बाल पहले जैसे धुंघराले बन जाते हैं।
![]()
तुम्हारी ऐन बुधवार, 28 जनवरी, 1944 मेरी प्यारी किट्टी, मैं तुम्हें हर रोज बासी खबरें सुनाती हूँ। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी की तरह नीरस लगेंगी। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे हर रोज वही बातें सुनानी पड़ती हैं। खाने के समय कभी-कभी राजनीति वाली बातें हो जाती हैं। कभी-कभी मझे अपनी मम्मी और वान दान की बचपन की बातें सननी पडती हैं जो हम हजार बा हैं। उधर डसेल हमें महँगे चॉकलेट, लीक करने वाली नौकाएँ, चार वर्षीय तैरने वाले बच्चे, रेस वाले घोड़े, पीड़ित माँसपेशियाँ और भयभीत मरीजों की कहानियाँ सुनाते हैं। हमें सभी किस्से याद हो गए हैं। अब कुछ नया सुनाने के लिए नहीं है। जब कोई बात करता है तो मैं बीच में टोकने का प्रयास नहीं करती। जॉन और मिस्टर क्लीमेन अज्ञातवास में छिपे लोगों की तकलीफें हमें सुनाते हैं।
जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। जो लोग कैद से मुक्त हो जाते हैं, उनकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। अज्ञातवास में रहना अब सामान्य-सी बात हो गई है। फ्री नीदरलैंड्स के लोग अपनी जान खतरे में डालकर अज्ञातवास में रहने वालों को धन की सहायता देते हैं। उनके लिए नकली पहचान-पत्र बनवाते हैं और ईसाई युवकों के लिए काम करते हैं। कुछ लोग हमारी भी सहायता कर रहे हैं। कुछ लोग जर्मनों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे हैं। कुछ हम जैसों की मदद कर रहे हैं। कुछ दिलचस्प बातें सुनने को मिली हैं। क्लीमेन ने बताया कि गेल्डरलैंड में पुलिसकर्मियों और भूमिगत लोगों के साथ फुटबॉल मैच हुआ। खुशी की बात है कि हिल्वरसम में भूमिगत लोगों को राशनकार्ड दिए गए। पर ये सब काम छिपकर किए जाते हैं।
तुम्हारी ऐन बुधवार, 29 मार्च, 1944-मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में यह घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने के बाद उन डायरी तथा पत्रों का संग्रह किया जाएगा, जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी है कि जब यह गुप्त एनेक्सी की कहानी छपेगी तो लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। हम लोगों के बारे में जानकारी पाकर लोग उत्सुक हो जाएँगे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि हवाई हमले के समय औरतें काफी डर जाती हैं। पिछले रविवार ब्रिटिश वायुसेना के 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुईडेन पर 550 टन बारूद के गोले बरसाए। उस समय हमारा मकान घास की पत्तियों के समान काँपता दिखाई पड़ रहा था। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यहाँ लोग लाइन बनाकर सामान खरीदते हैं।
चोरी का भय हमेशा बना रहता है। लोग हाथों में अंगूठियाँ नहीं पहनते। छोटे बच्चे भी चोरी करने लगे हैं। लोग चौराहे की घड़ियाँ तथा सार्वजनिक टेलीफोन भी उतार लेते हैं। डच लोग नैतिकता को छोड़ चुके हैं। सभी लोग भूख से परेशान हैं। हफ्ते का राशन सिर्फ दो दिन चलता है। बच्चे बीमारी तथा भूख से व्याकुल हो रहे हैं। फटे कपड़े तथा फटे-पुराने जूते पहनने पड़ते है। जूतों की मरम्मत के लिए चार-पाँच महीनों तक मोची की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लोगों को जर्मनी भेजा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों पर भी हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय और पुलिस अधिकारी लोगों की सहायता कर रहे हैं। यह गलत बात है कि लोग डच में गलत काम करते हैं।
तुम्हारी ऐन मंगलवार, 11 अप्रैल, 1944-मेरी प्यारी किट्टी, शनिवार का दिन है। 2 बजे के लगभग तेज गोलाबारी होने लगी। मशीनगर्ने भी चलने लगीं। रविवार को मेरे बुलाने पर पीटर साढ़े चार बजे मुझसे मिलने आया। हम ऊपर अटारी पर चले गए। उस समय रेडियो पर मोत्ज़ार्ट संगीत बज रहा था। हम दोनों एक पेटी पर सटकर बैठे हुए थे। मोश्ची भी हमारे साथ थी। पौने नौ बजे मिस्टर मिस्टर डसेल का कशन लेकर नीचे आ गए। इस पर डसेल हमसे नाराज हो गया। साढ़े नौ बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। पिताजी, वान दान और पीटर जल्दी से नीचे गए और मैं, माँ, मार्गोट और मिसेज वान दान ऊपर इंतजार करने लगीं। एक जोरदार धमाके से हम सभी औरतें डर गई। दस बजे जब पापा ऊपर आए, तब वह घबराए हुए थे।
तब उन्होंने आज्ञा दी कि हम बत्तियाँ बुझाकर ऊपर चली जाएँ। डर था कि पुलिस आ रही है। सभी आदमी नीचे थे। घर में घना काला अंधकार था। फिर से दो जोरदार धमाके हुए। पता चला कि गोदाम का आधा फाटक गायब था। होम गार्ड्स को सावधान कर दिया। वे चारों धीरे-धीरे नीचे गए। उन्होंने देखा कि गोदाम में सेंधमार अपने काम में लगे हुए थे। पुलिस के डर के कारण सेंधमार भाग गए थे। किसी प्रकार फाटक फिर से बंद कर दिया गया। इसी बीच एक आदमी और एक औरत पुलिस वहाँ पहुँच गए। सभी आदमी ऊपर बुककेस के पीछे छिप गए थे।
मंगलवार, 13 जून, 1944 मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं पंद्रह वर्ष की हो गई हूँ। जन्मदिन पर मुझे कलात्मक इतिहास की पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, बैल्टें, जैम की शीशी, रूमाल, दही के दो कटोरे, ब्रेसलेट, मिठाई, मीठे मटर, वनस्पति विज्ञान की पुस्तक, लिखने की कापियाँ, चीज के स्लाइस, मारिया लेरेसा की एक किताब और गुलदस्ता मिला है। इधर मौसम बड़ा खराब है। हमले अभी भी जारी हैं। जो फ्रांसीसी गाँव ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हो गए हैं, उन्हें देखने के लिए चर्चिल, स्मट्स आइजनहाबर तथा आर्मोल्ड आदि गए। इनमें चर्चिल बहुत ही बहादुर व्यक्ति है। ब्रिटिश सैनिक अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, परंतु हॉलैंड के लोग इस पक्ष में नहीं हैं कि वे ब्रिटिश पर कब्जा करें। वे चाहते हैं कि ब्रिटिश सैनिक लड़ाई करें और हॉलैंड को स्वतंत्र कराने के लिए खुद का बलिदान करें तथा आजादी मिलने पर माफी माँगते हुए हॉलैंड को छोड़कर चले जाएँ। इन्हें यह नहीं पता कि ब्रिटेन जर्मनी के साथ सुलह कर लेता तो हॉलैंड जर्मनी बन गया होता।
डच लोगों को यह समझाना जरूरी है कि जर्मन हमारे हमलावर हैं और ब्रिटेन हमारे रक्षक हैं। मैं हर समय विचारों में डूबी रहती हूँ। मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं तथा डाँट-फटकार भी सुननी पड़ती है। मुझे अपनी कमजोरियों और खामियों का पता है। मैं स्वयं को बदलना चाहती हूँ। सभी मुझे अक्खड़ मानते हैं। मिसेज वान दान और डसेल मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिसेज वान दान मुझसे भी अधिक अक्खड़ हैं। उनका कहना है कि मेरी पोशाकें छोटी हैं। उनकी अपनी पोशाकें भी छोटी पड़ गई हैं। वे मुझे तीसमारखाँ कहती हैं, जबकि वे मुझसे अधिक तीसमारखाँ हैं।
वे अकसर उन विषयों के बारे अधिक बोलती हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है लेकिन मैं बहुत कुछ जानती हूँ जब मैं अपनी तुलना किसी से करती हूँ तो अपने आप को धिक्कारने लगती हूँ। माँ के उपदेश सुन-सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। इससे मेरी कब मुक्ति होगी। मेरा विचार है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी भावनाओं को समझ सके। मेरा विचार है कि पीटर मुझे दोस्त समझकर प्यार करता है, गर्लफ्रेंड समझकर नहीं। उसका प्रेम हर दिन बढ़ता चला जा रहा है पर कोई रहस्यात्मक शक्ति हमें पीछे धकेल रही है।
मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं पीटर के पीछे प्रेम में दीवानी हो चुकी हूँ। जब मैं उससे नहीं मिलती तो परेशान हो जाती हूँ। पीटर एक भला लड़का है, पर उसके धर्म के प्रति विचार उचित नहीं हैं। वह हर समय खाने की बातें करता रहता है इसलिए हम दोनों ने निर्णय किया है कि हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वह बहुत शांतिप्रिय, सहनशील तथा बहुत-ही सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मेरी गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह चाहता है कि काम-काज में सही तरीका व सही सलीका हो। कोई उस पर आरोप न लगाए। परंतु वह अपने दिल की बात मुझसे नहीं बताता है। वह एक घुन्ना व्यक्ति है।
मैंने और पीटर ने कुछ दिन इकट्ठे एनेक्सी में बिताए हैं। हमने वर्तमान, भविष्य तथा भूतकाल की बातें की हैं। मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली। मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती हूँ। एक दिन गर्मी की रात के साढ़े ग्यारह बजे थे। मैं चाँद को देखना चाहती थी। बाहर चाँदनी की तीव्रता थी। इसलिए मैं खिड़की नहीं खोल पाई। अन्ततः एक दिन मैंने बरसात के समय खिड़की खोलकर रात में तेज हवाओं और बादलों को देखा। डेढ़ बरस में पहली बार मुझे यह मौका मिला था। .
आसमान, बादलों, चाँद, तारों को देखकर मुझे शांति मिलती है और आशा की भावना ने मुझको बोर कर दिया। शांति तो रामबाण दवा के समान है। प्रकृति के वरदान की समता कोई नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि पुराणों में शारीरिक क्षमता अधिक होती है। इसलिए वे औरतों पर आरंभ से शासन करते हैं। पुरुष कमाकर लाता है, बच्चों का पालन-पोषण करता है और जो मन में आए वही करता है। औरतें इस बेवकूफी का शिकार बनती हैं। परंतु यह प्रथा बहुत पुरानी पड़ चुकी है। अब शिक्षा, प्रगति और काम ने औरतों को जागृत कर दिया है। कुछ देशों में औरतों को पुरुषों के बराबर हक मिल चुके हैं, परंतु औरत आज पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। मेरा विचार है कि औरतों को भी पुरुषों को समान उचित सम्मान मिलना चाहिए।
औरतों को सैनिकों-सा कहीं अधिक यंत्रणा को सहन क दर्जा मिलना चाहिए। युद्ध में लड़ते समय सैनिक जिस पीड़ा और यत्रंणा को सहन करते हैं औरतें बच्चे को जन्म देते समय उससे को सहन करती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। परंत बच्चा पैदा करने के बाद औरत की संदरता नष्ट हो जाती है। औरत के कारण ही मानव जाति आगे बढ़ रही है। वह बहुत अधिक मेहनत करती है, पर पुरुष उसे उचित सम्मान नहीं देता। मेरा कहना है कि औरतों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिएँ। मैं ऐसे पुरुषों की निंदा करती हूँ जो समाज में औरतों के योगदान को महत्त्व नहीं देते। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रुइफ से पूरी तरह सहमत हूँ कि सभ्य समाज में औरतों द्वारा बच्चे पैदा करना अनिवार्य काम नहीं है क्योंकि औरत के समान पुरुष को इस तरह गुजरना नहीं पड़ता। मेरा विचार है कि अगली सदी तक यह धारणा बदल जाएगी कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। आने वाले समय में औरतों को अधिक सम्मान तथा आदर प्राप्त होगा।
तुम्हारी
ऐन फ्रैंक
कठिन शब्दों के अर्थ
अलसाई सी = आलस्य से युक्त। बिजनेस पार्टनर = व्यापार का साँझीदार। नज़ारे = दृश्य। हर्गिज़ = बिल्कुल। अज्ञातवास = छिपकर रहना। आतंकित = डरे हुए। कुलबुलाना = उथल-पुथल मचाना, व्याकुल होना। अफसोस = पछतावा। अजीबो-गरीब = विचित्र आश्चर्यजनक। स्मृति = यादें। पोशाक = पहनने वाले वस्त्र। मायने = अर्थ। स्टॉकिंग्स = लंबी जुराबें जो पूरी टाँगों को ढक लेती हैं। सन्नाटा = चुप्पी, मौन। अजनबी = अपरिचित। घोड़े बेचकर सोना = चिंता रहित सोना। किस्मत = भाग्य। बदन = शरीर। वजह = कारण। परवाह = चिंता करना। दिलचस्पी = रुचि । अरल्लम-गरल्लम = उल्टी-सीधी। बेचारगी = मजबूरी, लाचारी। निगाह = नज़र। वाहन = सवारी। दास्तान = विवरण, कथा। दौरान = मध्य, बीच में। यानी = अर्थात। गलियारा = संकरा रास्ता। दमघोंटू = साँस को रोकने वाला। पैसज = गलियारा। जरिया = द्वारा। सपाट = साधारण। बेडरूम = सोने का कमरा। स्टडीरूम = पढ़ने का कमरा। गुसलखाना = नहाने का कमरा। गरीबखाना = रहने का मकान। बखान = वर्णन। किस्सा = कहानी, वर्णन। राह देखना = इंतजार करना। अटा पड़ा = भरा हुआ। तरतीब = ढंग से, क्रमानुसार। पस्त = निढाल, थकी हुई।
![]()
ढह गए = गिर गए। फुर्सत = समय की कमी। इस्तेमाल = प्रयोग करना। किफायत = कम खर्चा करना। पखवाड़े = पंद्रह दिन का समय। अरसा = समय, वक्त। तरीका = उपाय। डिनर = रात का भोजन। दरअसल = वास्तव में। शेयर करना = भाग लेना। खरादेमाग = उल्टा-सीधा सोचने वाला, अक्खड़। तुनकमिजाज = जल्दी क्रोध करने वाला। वाकई = सचमुच। मीनमेख निकालना = कमियाँ निकालना। दुत्कारना-फटकारना = धमकाना। खामी = कमी। आसान = सरल। अजीब = विचित्र । ख्याल = विचार । तटस्थता = निष्पक्षता। भूमिगत = छिपकर रहना। अफवाह = झूठी बात। सुबूत = प्रमाण। हफ्ता = सत्ता। अनुमानित = लगभग। अदा करना = चुकाना। अदायगी = चुकाने की प्रक्रिया। फिलहाल = इस समय। गर्दन पानी के ऊपर होना = सुरक्षित होना, कुशलमंगल होना। कायदे-नियम = पत्राचार, पत्र-व्यवहार। कारोबार = व्यापार। सवाल-जवाब = प्रश्नोत्तर। सिलसिला = क्रम। महसूस करना = अनुभव करना। वंश वृक्ष = परिवार की वंशावली। खासी = अधिक। अतीत = गुजरा हआ समय। मेहरबान = दयाल । फरटि = तेजी से। फिकरा कसना = ताने म न होना। टोक देना = बीच में रोकना। फलाँ = अमुक। कान पकना = सुनने की इच्छा न होना।
जुगाली = बार-बार चबाने की प्रक्रिया। जरा = तनिक। हिमाकत = अशिष्टता। दिवाला पिटना = सारा धन समाप्त हो जाना। तकलीफ = कष्ट। हमदर्दी = सहानुभूति। प्रतिरोधी दल = मुकाबला करने वाला दल। वित्तीय = आर्थिक। रोजाना = हर रोज, प्रतिदिन। मनि खुशदिल = प्रसन्नचित्त। उपहार = भेंट। मदद = सहायता। दिलचस्प = रोचक। आग्रह = अनुरोध। मोची = जूतों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति। मर्द = पुरुष। आमंत्रण = बुलावा। अटारी = मकान की ऊपर की मंजिल का कमरा। खूबसूरत = सुंदर। दिव्य = अलौकिक। सटकर बैठना = पास-पास। खफा = नाराज। प्रहसन = हास्य नाटक। दाल में काला = कुछ गड़बड़ होना। सेंधमारी = चोरी करना। आशंका = डर। निगाह = नजर। ताला जड़ना = ताला लगाना। थरथराना = काँपना। निष्फल = बेकार। ढिठाई = धृष्टता। फटाफट = जल्दी, शीघ्र । जुटा नहीं पाना = व्यवस्था न कर पानी। उपहार = भेंट। जन्मजात = जन्म से, पैदायशी। ब्रिटिश = ब्रिटेन की सरकार। नफरत = घृणा। वाहियात = बेकार की बातें, बकवास। बुढ़ाते = वृद्ध व्यक्ति। प्रताड़ित करना = मारना, कष्ट देना। ताकत = शक्ति। सांत्वना = दिलासा देना, संतोष। आत्मीय = अपनापन। इल्ज़ाम = आरोप। घुन्ना = चुप रहने वाला। मंत्रमुग्ध = ध्यान में मग्न, वशीभूत । साक्षात्कार = भेंट, इंटरव्यू। उत्कट चाह = तीव्र अभिलाषा। सराबोर = पूर्ण करना। विनम्रता = शालीनता से। वाहियात = बेकार की बातें। स्वतंत्र = आजाद। सानी = मुकाबला। अलंकृत = सुशोभित। जनना = पैदा करने वाली। भर्त्सना = निंदा, चुगली। डींग हाँकना = झूठी प्रशंसा करना। हकदार = असली मालिक।
HBSE 12th Class Hindi Solutions Vitan Chapter 4 डायरी के पन्ने Read More »