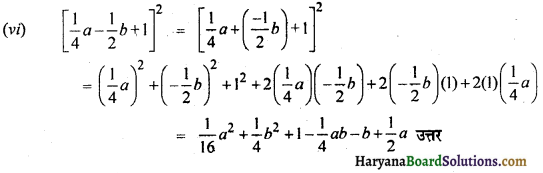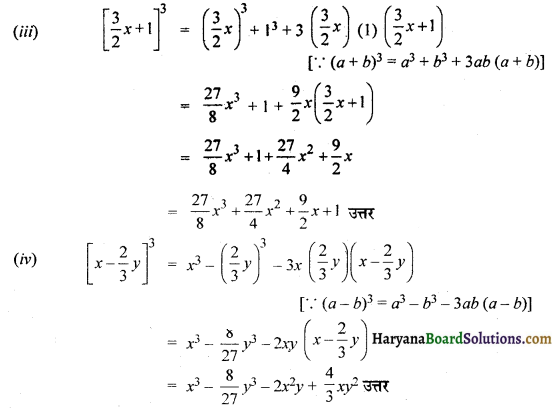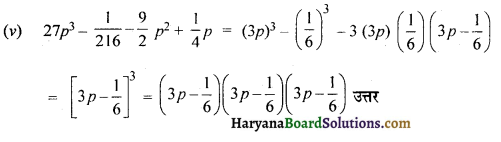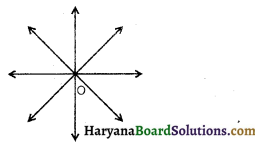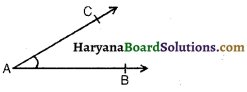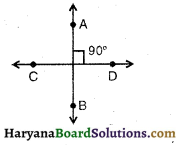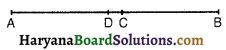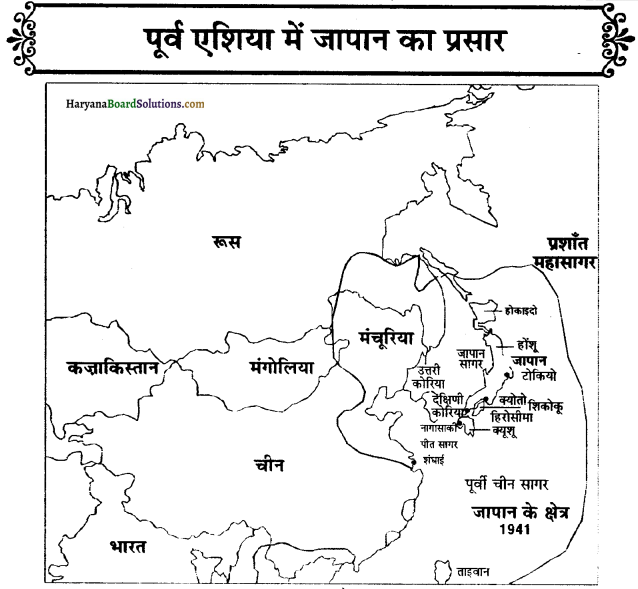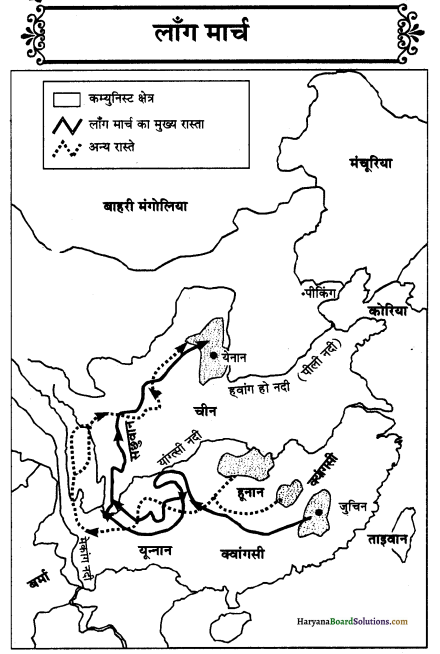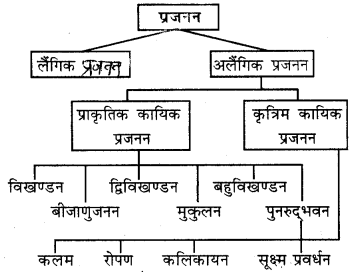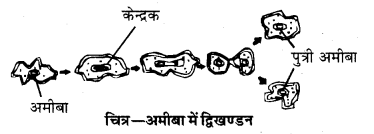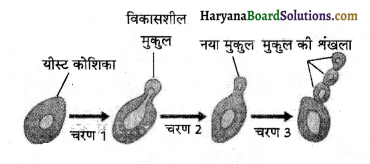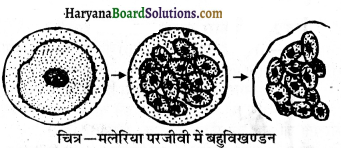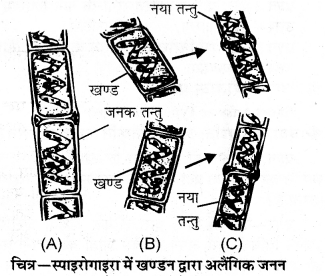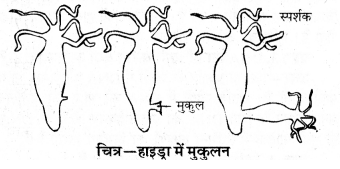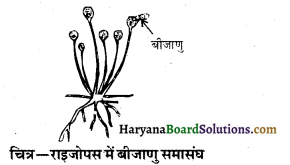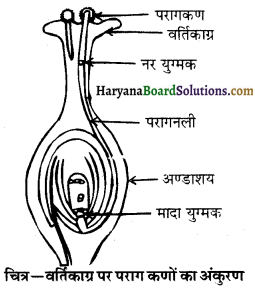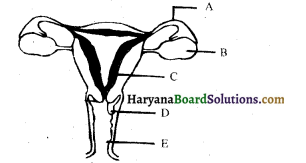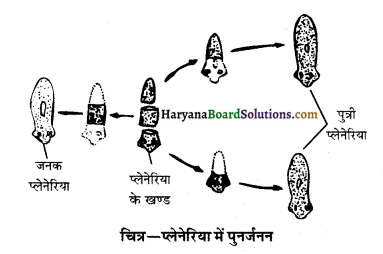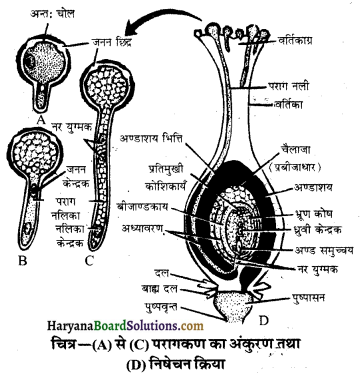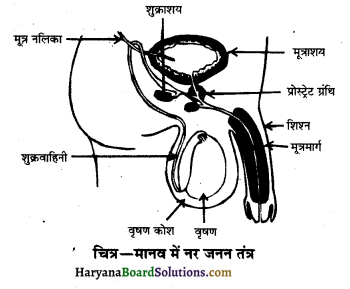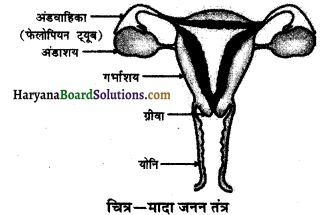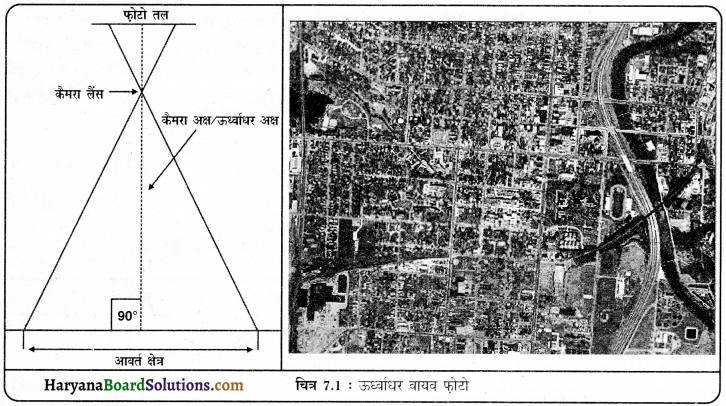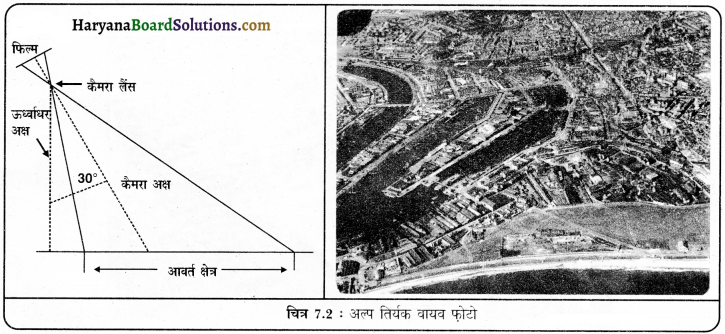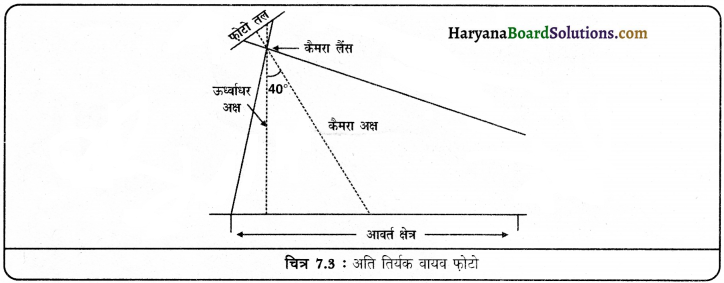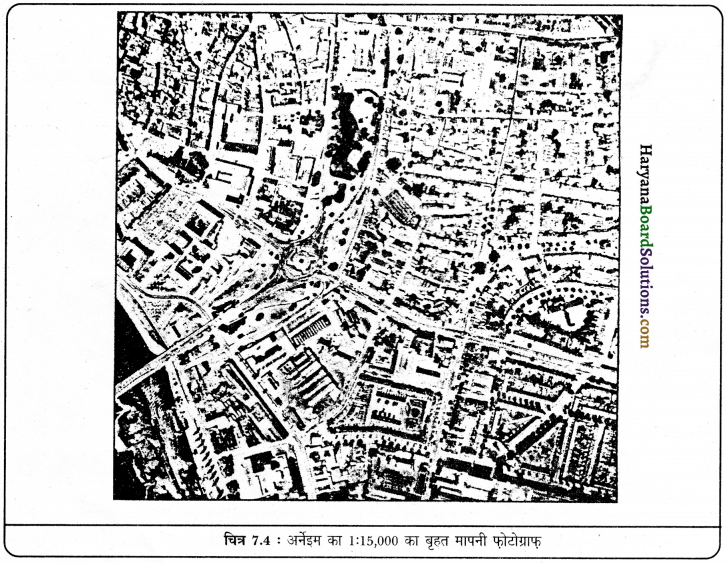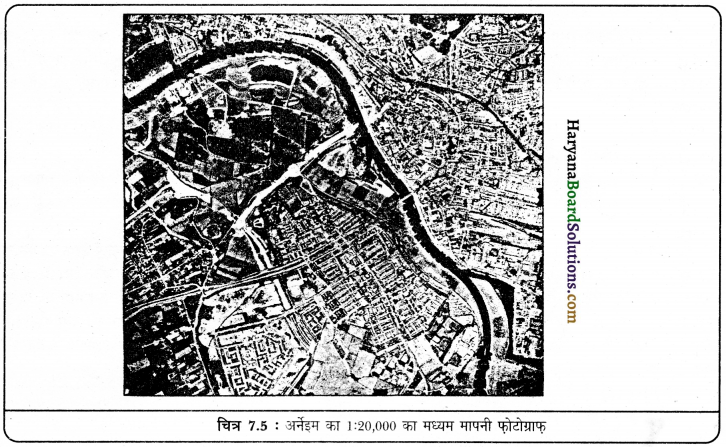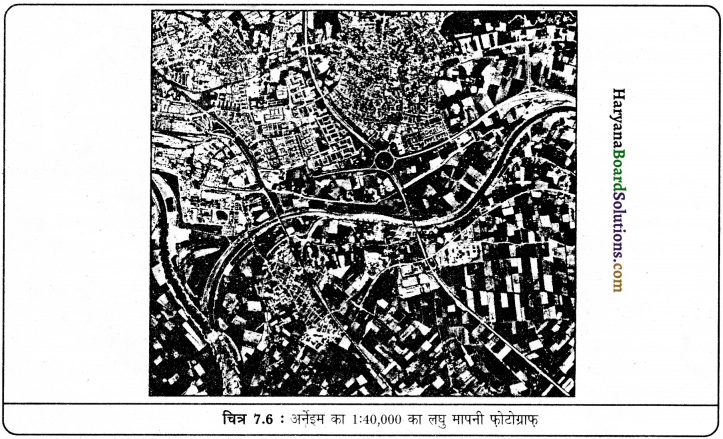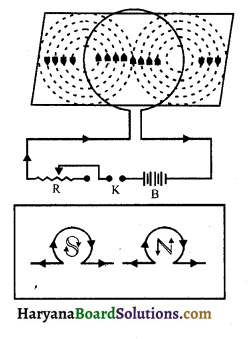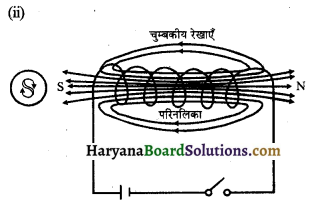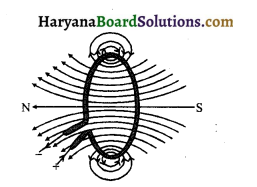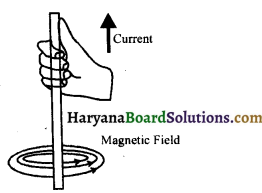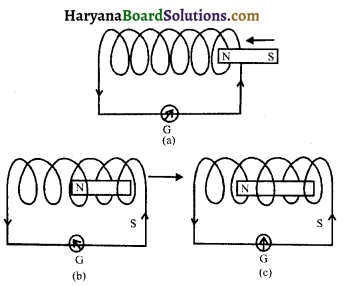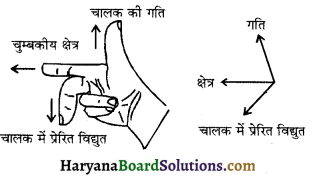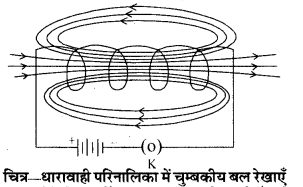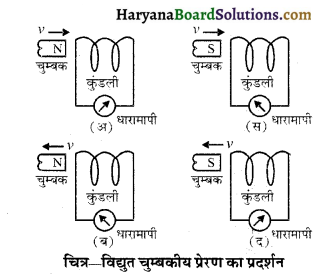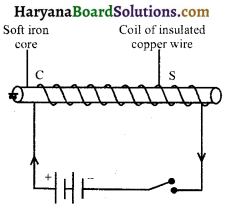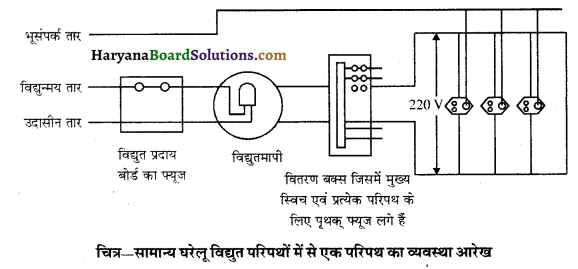Haryana State Board HBSE 11th Class History Important Questions Chapter 11 आधुनिकीकरण के रास्ते Important Questions and Answers.
Haryana Board 11th Class History Important Questions Chapter 11 आधुनिकीकरण के रास्ते
निबंधात्मक उत्तरों वाले प्रश्न
प्रश्न 1.
जापान में शोगुनों के उत्थान एवं पतन के बारे में आप क्या जानते हैं ? वर्णन कीजिए।
उत्तर:
जापान के इतिहास में शोगुनों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जापान का सम्राट मिकाडो (mikado) सर्वोच्च होता था। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। वह क्योतो (Kyoto) से शासन करता था। सम्राट का प्रधान सेनापति शोगन कहलाता था। जापान के राजनीतिक इतिहास में एक नए चरण का आरंभ तब हुआ जब 1603 ई० में तोकुगावा (Tokugawa) वंश के लोगों ने शोगुन पद पर अधिकार कर लिया। इस वंश के लोग इस पद पर 1867 ई० तक कायम रहे।
तोकुगावा शोगुनों ने अपनी शक्ति में काफी वृद्धि कर ली थी। उनके शासनकाल में सम्राट् बिल्कुल महत्त्वहीन हो गया था। कोई भी व्यक्ति शोगुन की अनुमति के बिना सम्राट से नहीं मिल सकता था। सम्राट को प्रशासन में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं दी गई थी। तोकुगावा शोगुनों ने एदो (Edo) को जिसे अब तोक्यो (Tokyo) के नाम से जाना जाता है अपनी राजधानी घोषित किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने विरोधियों को पराजित कर जापान में कानून व्यवस्था को लागू किया।
उन्होंने एदो में एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया जहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों को रखा जाता था। वे दैम्यो, प्रमुख शहरों एवं खदानों (mines) पर भी नियंत्रण रखते थे। उन्होंने जापान को 250 क्षेत्रों (domains) में बाँटा था। प्रत्येक क्षेत्र को एक दैम्यो (daimyo) के अधीन रखा गया था। दैम्यो अपने अधीन क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र होता था। उसे अपने अधीन क्षेत्र के लोगों को मृत्यु दंड देने का अधिकार था।
शोगुन दैम्यो पर कड़ा नियंत्रण रखते थे ताकि वे शक्तिशाली न हो जाएँ। उन्हें सैनिक सेवा करने एवं जन-कल्याण के कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। शोगुन के जासूस उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक दैम्यो के लिए यह आवश्यक था कि वह वर्ष के चार माह राजधानी एदो में रहे।
जापान के प्रशासन में सामुराई (samurai) की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। सामुराई योद्धा वर्ग (warrior class) से संबंधित थे। वे शोगुन एवं दैम्यो को प्रशासन चलाने में प्रशंसनीय योगदान देते थे। वे अपनी वफ़ादारी, वीरता एवं सख्त जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। केवल उन्हें तलवार धारण करने का अधिकार था। वे रणभूमि में वीरगति पाने को एक भारी सम्मान समझते थे। पराजित होने पर वे आत्महत्या कर लेते थे। आत्महत्या के लिए वे दूसरे समुदाय की तलवार से अपना पेट चीर लेते थे। इसे हरकारा (Harkara) पद्धति कहा जाता था।
उन्हें समाज का विशिष्ट वर्ग माना जाता था। अत: उन्हें अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई थीं। तोकुगावा शासनकाल (1603-1867 ई०) में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक स्तर पर अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए जिनके दूरगामी प्रभाव पड़े। 17वीं शताब्दी के अंत में तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिन्होंने आधुनिक जापान के विकास की आधारशिला रखी। प्रथम, किसानों से हथियार वापस ले लिए गए। केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इसके परिणामस्वरूप जापान में एक लंबे समय के पश्चात् शाँति स्थापित हुई।
दूसरा, दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए तथा उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने दिया गया। इससे जापान के विकास को बल मिला। तीसरा, जापान की भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इसका उद्देश्य भूमि के मालिकों तथा करदाताओं का निर्धारण करना था। कर निर्धारण भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर किया जाता था। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का शहर एदो (Edo) विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। उस समय एदो में 10 लाख से अधिक लोग रहते थे।
इसके अतिरिक्त ओसाका (Osaka), क्योतो (Kyoto) एवं नागासाकी (Nagasaki) जापान के अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। जापान में उस समय कम-से-कम 6 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। उस समय अधिकाँश यूरोपीय देशों में एक बड़ा शहर होता था। जापान में शहरों के तीव्र विकास से व्यापार एवं वाणिज्य को बहुत बल मिला। इससे व्यापारी वर्ग बहुत धनी हुआ। इस वर्ग ने जापानी कला एवं साहित्य को एक नई दिशा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
तोकुगावा काल में जापान के लोगों में शिक्षा का काफी प्रचलन था। अनेक लोग केवल लेखन द्वारा ही अपनी जीविका चलाते थे। पुस्तकों का प्रकाशन बड़े स्तर पर किया जाता था। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। वे किताबों की छपाई के लिए लकड़ी के ब्लॉकों का प्रयोग करते थे। लोगों में पढ़ाई का इतना शौक था कि वे पुस्तकों को किराए पर लेकर भी पढ़ते थे। 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया गया। इससे जापान के लोगों को पश्चिम के ज्ञान के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
तोकुगावा काल में जापान एक धनी देश था। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान चीन से रेशम तथा भारत से वस्त्र आदि विलासी वस्तुओं का आयात करता था। इसके बदले वह सोना एवं चाँदी देता था। इसका जापानी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण तोकुगावा को इन कीमती वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। उन्होंने रेशम के आयात को कम करने के उद्देश्य से 16वीं शताब्दी में निशिजन (Nishijin) में रेशम उद्योग की स्थापना की। आरंभ में केवल 31 परिवारों का एक संघ इस उद्योग से संबंधित था।
17वीं शताब्दी के अंत में इस संघ में 70,000 लोग सम्मिलित हो गए थे। इससे रेशम उद्योग को प्रोत्साहन मिला। 1713 ई० में केवल घरेलू धागे का प्रयोग करने संबंधी आदेश से इस उद्योग को अधिक बल मिला। 1859 ई० में जापान द्वारा विदेशी व्यापार आरंभ किए जाने से रेशम के व्यापार को सर्वाधिक मुनाफा मिलने लगा। इसका कारण यह था कि निशिजन का रेशम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। मुद्रा का बढ़ता हुआ प्रयोग तथा चावल का शेयर बाज़ार इस बात का संकेत था कि जापानी अर्थतंत्र नयी दिशाओं में विकसित हो रहा था।
1867 ई० में शोगुन पद की समाप्ति के साथ ही जापान के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। शोगुनों का पतन किसी अचानक घटना का परिणाम नहीं था। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. शोगुनों की पक्षपातपूर्ण नीति:
शोगुनों की नीति बहुत पक्षपातपूर्ण थी। उन्होंने राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर केवल तोकुगावा वंश के लोगों को ही नियुक्त किया। इसके चलते अन्य सामंती वंशों में निराशा फैली तथा उन्होंने शोगनों का अंत करने का प्रण किया।
2. गलत आर्थिक नीति :
शोगनों के शासनकाल में उनकी गलत नीतियों के चलते जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। विवश होकर उन्हें अपने व्यय में कटौती करनी पड़ी। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी सेना की संख्या में कुछ कमी कर दी। किंतु नौकरी से निकाले गए सैनिक इसे सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने शोगुनों को एक सबक सिखाने का निर्णय किया।
3. किसानों की दयनीय स्थिति:
शोगुन शासनकाल में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन पर अनेक प्रकार के कर लगाए गए थे। इन करों को बलपूर्वक वसूल किया जाता था। विवश होकर उन्होंने विद्रोहों का दामन थामा। इन विद्रोहों के चलते जापान में अराजकता फैल गयी थी।
4. व्यापारिक वर्ग का उदय:
19वीं शताब्दी जापान के समाज में एक नवीन व्यापारिक वर्ग का उत्थान हुआ। उन्नत व्यापार के चलते इनके पास काफी धन था। इसके बावजूद सामंत वर्ग उनसे ईर्ष्या करता था। अत: व्यापारी वर्ग अपनी हीन स्थिति को समाप्त करने के लिए जापान में शोगुन व्यवस्था का अंत करना चाहता था।
5. कॉमोडोर मैथ्यू पेरी का आगमन:
अमरीका ने 24 नवंबर, 1852 ई० को कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान की सरकार के साथ एक समझौता करने के लिए भेजा। वह 3 जुलाई, 1853 ई० को जापान की बंदरगाह योकोहामा में पहुँचा। इसका उद्देश्य अमरीका एवं जापान के मध्य राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। पेरी जापान की सरकार के साथ 31 मार्च, 1854 ई० को कानागावा की संधि करने में सफल हो गया।
इस संधि के अनुसार जापान की दो बंदरगाहों शीमोदा (Shimoda) एवं हाकोदाटे (Hakodate) को अमरीका के लिए खोल दिया गया। शीमोदा में अमरीका के वाणिज्य दूत को रहने की अनुमति दी गई। जापान ने अमरीका के साथ बहुत अच्छे राष्ट्र (most favoured nation) जैसा व्यवहार करने का वचन दिया। विदेशियों के प्रवेश से जापान में स्थिति ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया। शोगुन इस स्थिति को अपने नियंत्रण में लाने में विफल रहे। अतः उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ा।

प्रश्न 2.
मेज़ी काल के दौरान जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ ? वर्णन करें।
अथवा
मेज़ी काल के दौरान जापान के आधुनिकीकरण का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मेज़ी पुनर्स्थापना को जापान के इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है। 1868 ई० में मुत्सुहितो (Mutsohito) जापान का नया सम्राट बना। वह तोक्यो (Tokyo) में सिंहासनारूढ़ हुआ। मुत्सुहितो ने 1912 ई० तक शासन किया। उसने सिंहासन पर बैठते समय ‘मेज़ी’ की उपाधि धारण की थी। मेज़ी से अभिप्राय था प्रबुद्ध सरकार (Enlightened Government)। मेजी शासनकाल के दौरान जापान में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए गए।
इन सुधारों के चलते जापान की काया पलट हो गयी तथा वह एक शक्तिशाली एवं आधुनिक देश बन गया। वास्तव में मेज़ी पुनर्स्थापना के साथ जापान ने एक नए युग में प्रवेश किया। प्रसिद्ध इतिहासकार केनेथ बी० पायली के अनुसार, “मेज़ी काल (1868-1912) में जापान का पश्चिमीकरण अब तक का इतने कम समय हुआ किसी भी लोगों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है।”
1. सामंती प्रथा का अंत:
मेज़ी सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता जापान में सामंती प्रथा का अंत करना था । इससे पर्व संपर्ण जापान में सामंतों का बोलबाला था। वे अपने अधीन क्षेत्रों का शासन प्रबंध चलाते थे। इस संबंध में उन्हें व्यापक अधिकार प्राप्त थे। वे अपने अधीन क्षेत्रों के लोगों को मत्य दंड तक दे सकते थे। सेना में केवल सामुराई सामंतों को भर्ती किया जाता था। सामंतों के शक्तिशाली होने के कारण सम्राट् केवल नाममात्र का शासक रह गया था। सामंती प्रथा जापान के एकीकरण के मार्ग में सबसे प्रमुख बाधा थी।
सामंती प्रथा के चलते किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। सामंत उन पर घोर अत्याचार एवं भारी शोषण करते थे। मेज़ी सरकार ने 1871 ई० में जापान में सामंती प्रथा के अंत की घोषणा की। इसके अधीन सामंतों के सभी प्रकार के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। ऐसा करते समय सामंतों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। उनके लिए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की गई।
कुछ सामंतों को राष्ट्रीय सेना में भर्ती कर लिया गया। इस प्रकार जापान में सामंती प्रथा का अंत बिना किसी खून खराबे के हो गया। निस्संदेह इस प्रथा के अंत से जापान आधुनिकीकरण की दिशा की ओर अग्रसर हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० ए० बस के अनुसार, “सामंतवाद के अंत ने एक ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जो पिछले एक हजार वर्ष या इससे कुछ अधिक समय से जारी थी।”2
2. शिक्षा सुधार:
मेज़ी पुनर्स्थापना के पश्चात् जापान में उल्लेखनीय शिक्षा सुधार किए गए। इससे पूर्व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल समाज के उच्च वर्ग को ही प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा की ओर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। जापान में 1871 ई० में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से प्रगति हुई। संपूर्ण जापान में अनेक स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। 6 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।
विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनने एवं राष्ट्र के प्रति वफ़ादार रहने की प्रेरणा दी जाती थी। 1877 ई० में जापान में तोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम की प्रसिद्ध पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया। 1901 ई० में जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में एक मील पत्थर सिद्ध हुआ।
3. सैनिक सुधार:
मेज़ी काल में सेना को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए अब तक जापान में कोई राष्ट्रीय सेना नहीं थी। सम्राट् केवल सामंतों की सेना पर निर्भर करता था। इस सेना में कोई आपसी तालमेल नहीं था। इस सेना में केवल सामुराई वर्ग का प्रभुत्व था। 1853 ई० में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के जापान आगमन के समय जापानी सेना की कमज़ोर स्थिति स्पष्ट हो गई थी। अतः जापान की सुरक्षा के लिए इसकी सेना का पुनगर्छन करना अत्यंत आवश्यक था।
इस उद्देश्य से जापानी राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया । इसमें सभी वर्ग के लोगों को योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया। 1872 ई० में 20 वर्ष से अधिक नौजवानों के लिए सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। नौसेना (navy) को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया। सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया गया।
4. आर्थिक सुधार:
मेज़ी काल में जापानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रशंसनीय पग उठाए गए। सरकार ने फुकोकु क्योहे (Fukoku Kyohei) का नारा दिया। इससे अभिप्राय था समृद्ध देश एवं मज़बूत सेना।।
(1) औद्योगिक विकास:
जापान में उद्योगों के विस्तार की ओर सरकार ने अपना विशेष ध्यान दिया। इस उद्देश्य से 1870 ई० में जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना जापानी उद्योगों के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हआ। सरकार ने भारी उद्योगों के विकास के लिए पूँजीपतियों को प्रोत्साहित किया। अत: जापान में शीघ्र ही अनेक नए कारखाने स्थापित हुए।
इनमें लोहा-इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, जहाज़ उद्योग एवं शस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे। मित्सुबिशी (Mitsubishi) एवं सुमितोमो (Sumitomo) नामक कंपनियों को जहाज़ निर्माण के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं। इन उद्योगों में यूरोप से मँगवाई गई मशीनों को लगाया गया। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया।
(2) कृषि सुधार:
मेज़ी काल में कृषि क्षेत्र में भी प्रशंसनीय सुधार किए गए। सामंती प्रथा का अंत हो जाने से किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई। 1872 ई० में सरकार के एक आदेश द्वारा किसानों को उस भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। किसानों से बेगार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों को कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं।
उन्हें उत्तम किस्म के बीज दिए गए। पशओं की उत्तम नस्ल का प्रबंध किया गया। किसानों से अब अनाज की अपेक्षा नकद भू-राजस्व लिया जाने लगा। उन्हें कृषि के पुराने ढंगों की अपेक्षा आधुनिक ढंग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पश्चिमी देशों से अनेक कृषि विशेषज्ञों को जापान बुलाया गया। जापान में अनेक कृषि विद्यालयों की स्थापना की गई। उन प्रयासों के परिणामस्वरूप जापान के कृषि क्षेत्र में एक क्राँति आ गई। निस्संदेह इसे मेज़ी काल की एक महान् सफलता माना जा सकता है।
(3) कुछ अन्य सुधार:
जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेज़ी काल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। सर्वप्रथम यातायात के साधनों का विकास किया गया। 1870-72 ई० में जापान में तोक्यो (Tokyo) एवं योकोहामा (Yokohama) के मध्य प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। 1894-95 ई० में जापान में 2 हज़ार मील लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका था। जहाज़ निर्माण के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति की गई। द्वितीय, मुद्रा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। तीसरा, 1872 ई० में जापान में बैंकिंग प्रणाली को आरंभ किया गया। 1882 ई० में बैंक ऑफ जापान (Bank of Japan) की स्थापना की गई। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० यनागा के शब्दों में, “मेज़ी पुनर्स्थापना एक आर्थिक क्राँति थी।”
5. मेज़ी संविधान:
मेज़ी काल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 1889 ई० में एक नए संविधान को लागू करना था। इस संविधान के अनुसार सम्राट् को सर्वोच्च सत्ता सौंपी गई। उसे कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। संपूर्ण सेना उसके अधीन थी। उसे किसी भी देश से युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार दिया गया था। वह डायट (संसद्) के अधिवेशन को बुला सकता था तथा उसे भंग भी कर सकता था।
वह सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता था तथा वे अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। केवल सम्राट ही मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता था। डायट का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष तीन माह के लिए बुलाया जाता था। इसमें सदस्यों को बहस करने का अधिकार प्राप्त था। सम्राट् डायट की अनुमति के बिना लोगों पर नए कर नहीं लगा सकता था। नए संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे।
6. न्यायिक सुधार:
मेज़ी काल में अनेक न्यायिक सुधार भी किए गए। जापान में 1882 ई० में एक नई दंड संहिता को लागू किया गया। इसके अनुसार अपराधियों को क्रूर सजाएँ देना बंद कर दिया गया। न्यायालयों के अधिकार निश्चित कर दिए गए। दीवानी एवं फ़ौजदारी कानूनों को अलग-अलग परिभाषित किया गया। केवल ईमानदार एवं उच्च चरित्र के व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। अपराधियों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से नई जेलों का निर्माण किया गया। इस प्रकार जापान न्यायिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के पथ पर आगे अग्रसर हुआ।
7. रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव:
मेज़ी काल में जापानियों की रोज़मर्रा की जिंदगी में अनेक महत्त्वपूर्ण बदलाव आए। इसमें जापान में हुए तीव्रता से शिक्षा के प्रसार, जापानियों की पश्चिमीकरण में दिलचस्पी एवं पत्रकारिता के प्रचार ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मेज़ी काल से पूर्व जापान में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था।
इसके अधीन परिवार की कई पीढ़ियाँ परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थीं, मेजी में परिवार के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में तीव्रता से परिवर्तन आने लगा। अब एकल परिवार का प्रचलन बढ़ने लगा। इसमें पति, पत्नी एवं उनके बच्चे रहते थे। अतः वे नए घरों जिसे जापानी में होमु (homu) कहते थे में रहने लगे।
वे घरेलू उत्पादों के लिए बिजली से चलने वाले कुकर, माँस एवं मछली भूनने के लिए अमरीकी भूनक (American grill) तथा ब्रेड सेंकने के लिए टोस्टर का प्रयोग करने लगे। जापानियों में अब पश्चिमी वेशभूषा का प्रचलन बढ़ गया। वे अब सूट एवं हैट डालने लगे। औरतों के लिबास में भी परिवर्तन आ गया। वे यूरोपीय ढंग से अपने बालों को सजाने लगीं।
वे अब सौंदर्य वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देने लगीं। दाँतों की चमक-दमक के लिए टूथब्रश एवं ट्थपेस्ट का प्रचलन बढ़ गया। परस्पर अभिवादन के लिए हाथ मिलाने का प्रचलन लोकप्रिय हो गया। मनोरंजन के नए साधनों का विकास हुआ। लोग ट्रामों एवं मोटरगाड़ियों द्वारा सैर-सपाटों पर जाने लगे।
1878 ई० में जापान में लोगों के लिए भव्य बागों का निर्माण किया गया। लोगों की सुविधा के लिए विशाल डिपार्टमैंट स्टोर बनने लगे। 1899 ई० में जापान में सिनेमा का प्रचलन आरंभ हुआ। संक्षेप में मेज़ी काल में लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० लाटूरेट का यह कहना ठीक है कि, “19वीं शताब्दी के दूसरे मध्य में जापान ने उल्लेखीय परिवर्तन देखे।”
प्रश्न 3.
1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध के क्या कारण थे? इसके क्या परिणाम निकले?
अथवा
1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ? चर्चा कीजिए।
अथवा
शिमोनोस्की की संधि क्यों व कब हुई ? इसके क्या परिणाम निकले? इसके क्या परिणाम निकले?
उत्तर:
1894-95 ई० में जापान तथा चीन के मध्य एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का मूल कारण कोरिया था। इस युद्ध में जापान ने चीन को बहुत शर्मनाक पराजय दी। परिणामस्वरूप चीन के सम्मान को भारी आघात पहुँचा और जापान विश्व के शक्तिशाली देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ।
चीन-जापान युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. रूस की कोरिया में रुचि:
रूस की दक्षिणी पूर्वी सीमा कोरिया के साथ लगती थी। अत: उसने कोरिया पर अपना अधिकार करने की योजना बनाई। रूस ने कोरिया की सेना को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से अपने सैनिक अधिकारियों को वहाँ भेजा। इसके बदले में कोरिया ने लजरफ की बंदरगाह रूस को दे दी। अब रूस के जहाज़ बिना किसी बाधा के इस बंदरगाह पर आ-जा सकते थे। इस प्रकार कोरिया में रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। रूस के कोरिया में बढ़ते हुए प्रभाव को जापान सहन करने को तैयार नहीं था।
2. कोरिया की आंतरिक दशा शोचनीय:
कोरिया की आंतरिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह एक निर्बल देश था। उस समय कोरिया में अशांति फैली हुई थी तथा अव्यवस्था व्याप्त थी। वहाँ जापान यह अनुभव करता था कि कोरिया की यह आंतरिक स्थिति अन्य देशों के लिए एक नियंत्रण का कार्य कर सकती है। उसे सदैव यह भय लगा रहता था कि कोई अन्य देश कोरिया पर अपना अधिकार न कर ले। चीन भी अपने वंशानुगत अधिकार के कारण किसी अन्य देश के कोरिया में हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकता था। इन परिस्थितियों में चीन तथा जापान में युद्ध होना अनिवार्य था।
3. कोरिया में विदेशी शक्तियों का आगमन:
कोरिया में जापान के बढ़ रहे प्रभाव को देख कर चीन बहुत चिंतित हो गया। जापान के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उसने विदेशी शक्तियों को कोरिया में व्यापार करने के प्रयासों में अपना समर्थन दिया। परिणामस्वरूप अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस तथा फ्राँस आदि देशों ने कोरिया से संधियाँ की तथा अपने लिए अनेक सुविधाएँ प्राप्त की।
विदेशी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव से जापान घबरा उठा। अतः जापान कोरिया को विदेशी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त करवाना चाहता था ताकि उसकी स्वयं की स्वतंत्रता कायम रहे। इन परिस्थितियों में उसका चीन के साथ युद्ध अनिवार्य था।
4. 1885 ई० की संधि:
1885 ई० में जापान ने चीन के साथ एक संधि की। संधि के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए कि वे दोनों ही कोरिया से अपनी सेनाएँ वापस बुला लेंगे। इस संधि से चीन के कई राजनीतिज्ञ असंतुष्ट हो गए। चीनी राजनीतिज्ञों का विचार था कि कोरिया चीन का ही एक अंग है तथा चीन को कोरिया में अपनी सेनाएँ रखने का पूर्ण अधिकार है। चीन के इस विचार को जापान सहन करने को तैयार नहीं था। अतः चीन-जापान के मध्य युद्ध अनिवार्य था।
5. जापान के आर्थिक हित:
चीन-जापान यद्ध के कारणों में एक कारण कोरिया में जापान के आर्थिक हित भी थे। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वह कोरिया की ओर ललचाई नज़रों से देख रहा था । जापान में औद्योगिक विकास आश्चर्यजनक गति से हुआ था। अब उसे अपने तैयार माल तथा कच्चे माल के लिए मंडियों की आवश्यकता थी। अपने इस उद्देश्य के लिए जापान कोरिया को उपयुक्त स्थान समझता था। इसे चीन बिल्कुल भी सहन करने को तैयार नहीं था।
6. तात्कालिक कारण:
कोरिया में ‘तोंगहाक’ (Tonghak) संप्रदाय द्वारा किया गया विद्रोह चीन-जापान युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इस संप्रदाय के लोग विदेशियों को पसंद नहीं करते थे। कोरिया सरकार इस संप्रदाय के विरुद्ध थी तथा उसने एक अध्यादेश द्वारा इसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1883 ई० में इस संप्रदाय के नेताओं ने उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की माँग की।
परंतु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोरिया में प्रत्येक स्थान पर विद्रोह होने लगे। आरंभ में सरकार ने इस विद्रोह का दमन कर दिया किंतु 1894 ई० में इसने भीषण रूप धारण कर लिया। विवश होकर कोरिया की सरकार ने चीन एवं जापान से सैनिक सहायता माँगी।
परंतु इन सेनाओं के पहुंचने से पहले ही विद्रोह का दमन कर दिया गया था। कोरिया सरकार ने दोनों सरकारों को अपनी-अपनी सेनाएँ वापस बुलाने की प्रार्थना की। परंतु दोनों देशों ने अपनी सेनाएँ वहाँ से न निकाली। जापानी सेनाओं ने कोरिया के राजा को बंदी बना लिया और वहाँ की सरकार का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित सरकार ने जापान से आग्रह किया कि वह चीन की सेनाओं को कोरिया से मार भगाए। इस प्रकार 1 अगस्त, 1894 ई० को यह युद्ध आरंभ हो गया।
युद्ध से पूर्व ही जापान ने अपनी सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन कर लिया था। परंतु चीन की सेना इतनी कुशल नहीं थी तथा उसका लड़ने का ढंग भी प्राचीन ही था। यह युद्ध 9 मास तक चला। इस युद्ध में जापान को शानदार विजय प्राप्त हुई। 16-17 सितंबर, 1894 ई० को जापान ने पिंगयांग तथा यालू के युद्धों में चीन की सेनाओं को पराजित कर दिया तथा चीन की सेनाओं को कोरिया से खदेड़ दिया। फिर उसने मंचूरिया पर आक्रमण किया तथा लिआयोतुंग प्रायद्वीप की ओर चल पड़ा। जापानी सेनाओं ने तेलियनवैन तथा पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर लिया।
जापानी सेनाओं ने फ़रवरी 1895 ई० तक शातुंग तथा वी-हाई-वी पर भी अधिकार कर लिया। परिस्थितिवश चीन जापान के साथ समझौता करने के लिए विवश हुआ। अत: 17 अप्रैल, 1895 ई० को दोनों पक्षों में शिमोनोसेकी की संधि हुई जिसके परिणामस्वरूप युद्ध का अंत हुआ। युद्ध में पराजित होने के पश्चात् माँचू सरकार ने ली-हुंग-चांग को संधि के लिए जापान भेजा। ली-हुंग-चांग ने 17 अप्रैल, 1895 ई० को जापानी अधिकारियों के साथ शिमोनोसेकी की संधि की। इस संधि की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित अनुसार थीं-.
- चीन ने कोरिया को एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी।
- चीन ने पोर्ट आर्थर, फारमोसा, पेस्काडोरस तथा लियाओतुंग जापान को दे दिए।
- चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को 2 करोड़ तायल देगा।
- चीन जापान को सर्वाधिक प्रिय देश स्वीकार करेगा।
- चीन जापान के व्यापार के लिए अपनी चार बंदरगाहें शांसी, सो चाऊ, चुंग-किंग तथा हंग चाओ खोलेगा।
- जब तक चीन युद्ध की क्षतिपूर्ति की राशि जापान को नहीं चुकाएगा उसकी वी-हाई-वी नामक बंदरगाह जापान के पास रहेगी।
शिमोनोसेकी की संधि के कागजों पर अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसके 6 दिन पश्चात् ही फ्राँस, रूस तथा जर्मनी ने जापान को कहा कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीप चीन को लौटा दे। क्योंकि उन्हें भय था कि यदि लियाओतुंग पर जापान का अधिकार हो गया तो इससे चीन को निरंतर खतरा रहेगा तथा कोरिया की स्वतंत्रता भी स्थायी नहीं रह पाएगी। विवश होकर जापान ने शिमोनोसेकी की संधि में संशोधन करना मान लिया। उसने लियाओतुंग प्रायद्वीप चीन को वापस कर दिया तथा इसके बदले चीन से 3 करोड तायल की अतिरिक्त धन-राशि ले ली।
चीन-जापान युद्ध में जापान ने शानदार विजय प्राप्त की तथा चीन की शर्मनाक पराजय हुई। इस युद्ध में एक छोटे से बौने (जापान) ने एक दैत्य (चीन) को पराजित किया था। इस युद्ध से दोनों देश बहुत प्रभावित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार एच० एफ० मैकनैर के अनुसार, “यह वास्तव में जापान को प्रथम चुनौती थी।”5 संक्षेप में इन प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि:
जापान एशिया का एक छोटा सा देश था तथा चीन सबसे बड़ा देश था। फिर भी जापान ने चीन को पराजित कर दिया। इस युद्ध में विजय से जापान की प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गए। सभी यूरोपीय शक्तियों को विश्वास था कि जापान पराजित होगा। परंतु उसकी विजय ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। परिणामस्वरूप उसकी शक्ति की धाक् सारे विश्व में बैठ गई। प्रसिद्ध इतिहासकार एम०ई० कैमरन के अनुसार, “जापान के हाथों चीन की पराजय के महान् एवं दूरगामी प्रभाव पड़े।”
2. चीन की प्रतिष्ठा को गहरा आघात:
जापान ने जो कि एशिया का एक छोटा सा देश था, चीन जैसे बड़े देश को पराजित कर संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया था। चीन की इस घोर पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी० वी० राव का यह कहना ठीक है कि, “चीन के लिए पराजय एवं अपमानजनक संधि ने माँचू वंश के पतन का डंका बजा दिया।”
3. चीन की लूट आरंभ:
जापान के हाथों पराजित होने से चीन की दुर्बलता सारे विश्व के आगे प्रदर्शित हो गई। इस कारण यूरोपीय शक्तियों की मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। पहले पश्चिमी देशों ने चीन से कई प्रकार की रियायतें प्राप्त की हुई थीं। परंतु अब वे उसके साम्राज्य का विभाजन चाहने लगीं। अतः ये सभी देश चीन की लूट में जापान के भागीदार बनने के लिए तैयार हो गए। प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० लाटूरेट के अनुसार, “जापान द्वारा चीनी साम्राज्य के हिस्से को हड़पने की कार्यवाही से लूट की प्रक्रिया तीव्र हो गई।”
4. चीन में सुधार आंदोलन:
चीन की अपमानजनक पराजय से चीन के देशभक्त बड़े दुःखी हुए। वे अनुभव करने लगे कि चीन को भी जापान की भाँति आधुनिक ढंग के सुधार करने चाहिएँ। परंतु उस समय के माँचू शासक बड़े रूढ़िवादी थे। अतः वे इन सुधारों के पक्ष में नहीं थे। परिणामस्वरूप चीन में माँचू विरोधी सुधार आंदोलन चल पड़ा।
5. आंग्ल-जापानी समझौते की आधारशिला:
चीन जापान युद्ध के परिणामस्वरूप आंग्ल-जापानी समझौते की नींव रखी गई। जब जापान इस युद्ध में विजयी हो रहा था तो इंग्लैंड के समाचार-पत्रों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उनके अनुसार इंग्लैंड और जापान के हित सामान्य थे। अतः वे जापान को भविष्य का उपयोगी मित्र मानने लगे। जापान भी इंग्लैंड से मित्रता करना चाहता था। इस प्रकार ये दोनों देश एक-दूसरे के निकट आए तथा 1902 ई० में एक समझौता किया।
6. जापान-रूस शत्रुता:
शिमोनोसेकी की संधि के पश्चात् रूस जापान के विरुद्ध हो गया। उसने फ्राँस तथा जर्मनी के साथ मिल कर जापान पर दबाव डाला कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीय चीन को वापस कर दे। इससे जापान रूस से नाराज़ हो गया। इसके अतिरिक्त चीन-जापान युद्ध के पश्चात् जापान भी रूस के समान दूर-पूर्व में एक शक्ति के रूप में उभरा। दोनों देश महत्त्वाकांक्षी थे और यही महत्त्वाकांक्षा उन्हें 1904-05 के युद्ध की ओर ले गई।
प्रश्न 4.
रूस-जापान युद्ध 1904-05 के क्या कारण थे? इस युद्ध के क्या प्रभाव पड़े?
अथवा
रूस-जापान युद्ध 1904-05 के बारे में आप क्या जानते हैं ? इस युद्ध में जापान की सफलता के क्या कारण थे?
अथवा
रूस-जापान युद्ध के कारणों का वर्णन करो।
उत्तर:
सुदूर पूर्व में रूस तथा जापान दो महान् शक्तियाँ थीं। ये दोनों शक्तियों महत्त्वाकांक्षी थीं। ये दोनों शक्तियाँ साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करती थीं तथा इस नीति पर चलते हुए अपने-अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थीं। इसी कारण उनमें 1904-05 ई० में एक युद्ध हुआ जिसमें रूस पराजित हुआ और जापान को गौरवपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
I. रूस-जापान युद्ध के कारण
रूस-जापान युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. जापान के विरुद्ध रूस का हस्तक्षेप:
1894-95 ई० में हुए चीन-जापान युद्ध में जापान ने चीन को पराजित करके एक शानदार विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के पश्चात् हुई शिमोनोसेकी की संधि के अनुसार चीन ने अपने कुछ क्षेत्र जापान को दे दिए थे। इन प्रदेशों में एक लियाओतुंग प्रदेश भी था। उधर रूस भी अपने स्वार्थी हितों के कारण इन प्रदेशों पर नजर लगाए बैठा था।
इस कारण इस संधि के कुछ दिन पश्चात् ही उसने जापान पर दबाव डाला कि वह लियाओतुंग प्रदेश चीन को वापस कर दे। फ्राँस तथा जर्मनी ने भी रूस का समर्थन किया। अतः जापान को बाध्य होकर लियाओतुंग का प्रदेश चीन को वापस करना पड़ा। जापान रूस से अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था।
2. रूस-चीन गठबंधन:
लियाओतुंग का प्रदेश वापस मिलने पर चीन और रूस के संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए। रूस ने फ्रांस के साथ मिल कर एक बड़ी राशि चीन को ऋण स्वरूप दी। 1896 ई० में उसने चीन के साथ एक रक्षात्मक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के अनुसार उन्होंने यह निश्चित किया कि यदि जापान रूसी प्रदेशों अथवा चीन और कोरिया पर आक्रमण करता है तो वे सम्मिलित रूप से उसका सामना करेंगे। चीन तो जापान का शत्रु था ही, अपितु यह गठबंधन बन जाने से जापान का रूस के विरुद्ध होना स्वाभाविक था।
3. लियाओतुंग पर रूस का कब्जा:
चीन में हुए ‘रियायतों के लिए संघर्ष’ (scramble for concessions) में रूस सबसे महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल रहा था। अन्य रियायतों के साथ-साथ उसने 1898 ई० में लियाओतुंग का प्रदेश भी चीन से पट्टे पर ले लिया था। रूस की इस कार्यवाही से जापान भड़क उठा था क्योंकि यही प्रदेश उसने जापान से चीन को वापस दिलवाया था और अब उस पर कब्जा कर बैठा था। निस्संदेह इसने आग में घी डालने का कार्य किया।
4. मंचूरिया की समस्या:
मंचूरिया भी रूस-जापान युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना। मंचूरिया चीन के उत्तरी भाग में स्थित था तथा ये दोनों देश उसमें रुचि रखते थे। लियाओतुंग पर कब्जा करने के पश्चात् रूस ने पोर्ट आर्थर को अपना शक्तिशाली समुद्री अड्डा बनाने का प्रयास किया। उसने मंचूरिया में रेलवे लाइनें भी बिछाई। मंचूरिया में जापान के भी आर्थिक हित थे। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसके हितों को खतरा पैदा हो गया।
बॉक्सर विद्रोह के बाद भी रूसी सेनाएँ मंचूरिया में ही थीं। वहाँ से सेना हटाने की अपेक्षा उसने चीनी सरकार से और रियायतें प्राप्त करनी चाहीं परंतु जापान तथा इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। 1902 ई० में रूस ने वचन दिया कि वह 18 मास में अपनी सेनाएँ चीन से निकाल लेगा परंतु उसने ऐसा न किया। अतः जापान ने रूस को एक सबक सिखाने का निर्णय किया।
5. कोरिया की समस्या:
1894-95 ई० में हुए चीन-जापान युद्ध का मुख्य कारण कोरिया ही था। जापान ने इस यद्ध द्वारा कोरिया में चीन की प्रभसत्ता समाप्त कर दी थी। इस यद्ध के पश्चात रूस ने कोरिया पर जापान के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। परंतु रूस ने उत्तरी कोरिया के जंगलों से लकड़ी काटने का सिलसिला बंद न किया। इस के अतिरिक्त उसने इस क्षेत्र में सेना भी भेजनी आरंभ कर दी थी। जापान की सरकार ने इस का विरोध दर्शाते हुए एक पत्र रूसी सरकार के पास भेजा। परंतु रूसी सरकार ने इसकी कोई परवाह न की। परिणामस्वरूप इसने स्थिति को विस्फोटक बना दिया।
6. इंग्लैंड-जापान गठबंधन :
1902 ई० में जापान तथा इंग्लैंड ने एक गठबंधन किया। इसके अधीन दोनों ने एक-दूसरे को वचन दिया कि चीन और कोरिया में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक-दूसरे को सहायता देंगे। संधि के अनुसार इंग्लैंड ने यह भी वचन दिया कि यदि रूस और जापान में युद्ध होता है तो वह निष्पक्ष रहेगा। परंतु यदि इस युद्ध में फ्राँस रूस की सहायता करेगा तो वह जापान का साथ देगा। इंग्लैंड के इस आश्वासन से जापान को प्रोत्साहन मिला और उसने रूस के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। जापान का यह व्यवहार भी इस युद्ध का कारण बना।
7. जापान द्वारा संधि के प्रयास:
जापान रूस की विस्तारवादी नीति से बड़ा चिंतित था। वह कोरिया तथा मंचूरिया के प्रश्न पर रूस से कोई समझौता करना चाहता था। अतः इन देशों के मध्य 1903 ई० में बातचीत आरंभ हुई जो कि फ़रवरी, 1904 ई० तक चली। जापान चाहता था कि यदि रूस कोरिया पर जापान का आधिपत्य स्वीकार कर ले तो वह मंचूरिया पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लेगा। परंतु यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर न पहुँच सकी। अंततः दोनों के मध्य 10 फ़रवरी, 1904 ई० को युद्ध आरंभ हो गया।
II. युद्ध की घटनाएँ
रूस-जापान युद्ध स्थल तथा समुद्र दोनों में लड़ा गया था। जापान के एडमिरल तोजो ने युद्ध का आरंभ करते हुए सबसे पहले पोर्ट आर्थर को चारों ओर से घेरा डाला। इसी समय जापानी सेनाओं ने रूस के स्थल मार्ग से आक्रमण किया। इस प्रकार जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर को स्थल तथा जल दोनों मार्गों द्वारा घेर लिया। रूस इस घेरे को तोड़ न सका। 10 महीनों के घेराव के बाद जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया।
यहाँ से जापानी सेनाएँ लियाओतुंग (Liaotung) की ओर बढ़ी तथा उसे भी विजय कर लिया। फ़रवरी, 1905 ई० को जापानी सेनाओं ने मंचूरिया की राजधानी मुकदेन (Mukaden) पर धावा बोल दिया। एक भयंकर युद्ध के पश्चात् रूसी सेनाएँ पराजित हुईं। रूसी सेनाएँ मुकदेन छोड़ कर भाग गईं तथा उन्होंने मंचूरिया में जापान का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। रूस के ज़ार ने अब समुद्री युद्ध में अपने हाथ आजमाने चाहे।
उसने अपनी नौसेना को बाल्टिक सागर से प्रशाँत सागर में भेजा ताकि पोर्ट आर्थर पर फिर से अधिकार किया जा सके। जब यह सेना तुशिमा (Tsushima) पहुँची तो जापानी एडमिरल तोजो (Admiral Tojo) ने इसे तहस-नहस कर दिया। इस निर्णायक लड़ाई में जापान विजयी रहा। अब तक रूस तथा जापान दोनों ही इस लड़ाई से तंग आ चुके थे। इस युद्ध के कारण जापान पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा था तथा रूस की कठिनाइयाँ भी बहुत बढ़ गई थीं।
अब वे किसी संधि के लिए सोचने लगे थे। इस कार्य में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) ने मध्यस्थता की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को शाँति संधि की शर्ते निर्धारित करने के लिए पोर्टसमाउथ बुलाया गया। काफी वाद-विवाद के पश्चात् । सितंबर, 1905 ई० को दोनों पक्षों में पोर्टसमाउथ की संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया।
पोर्टसमाउथ की संधि (Treaty of Portsmouth) संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के प्रयत्नों के फलस्वरूप रूस तथा जापान के मध्य 5 सितंबर, 1905 ई० को एक संधि हुई। इसे पोर्टसमाउथ की संधि कहा जाता है। इस संधि की शर्ते निम्नलिखित थीं
(1) कोरिया में जापान के राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक हितों को रूस ने स्वीकार कर लिया।
(2) पोर्ट आर्थर तथा लियाओतुंग के प्रायद्वीप जापान को मिल गए।
(3) इस संधि में यह भी कहा गया कि रूस तथा जापान दोनों ही मंचूरिया से अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। केवल रेलों की रक्षा के लिए ही कुछ सैनिक वहाँ रहेंगे।
(4) दोनों ने माना कि मंचूरिया में रेलों का उपयोग केवल व्यापारिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
(5) आपान को स्खालिन द्वीप का दक्षिण भाग प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकारों एफ० एच० माइकल एवं जी०ई० टेलर के शब्दों में, “पोर्टसमाउथ की संधि ने जापान को एशिया में एक महाद्वीपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया।
III. जापान की सफलता के कारण
रूस-जापान युद्ध में जापान की सफलता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
(1) जापानी सैनिक तथा जनता दोनों ही देश-भक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। सारा राष्ट्र जापान की सरकार के साथ था तथा देश के लिए मर मिटने को तैयार था। उन्होंने शत्रु को हराने के लिए तन, मन तथा धन से सरकार की सहायता की। यही राष्ट्र-भक्ति की भावना जापानियों की विजय का मूल कारण थी।
(2) जापान ने अपनी सेना का आधुनिक ढंग से पुनर्गठन कर इसे काफी शक्तिशाली. बना लिया था। इस शक्तिशाली सेना के आगे रूसी सेनाएँ टिक न सकीं।
(3) जापान ने युद्ध के आरंभ होने से पूर्व ही अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने यातायात के साधनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं का भी उचित प्रबंध किया जो उसकी विजय में सहायक सिद्ध हुईं।
(4) तोजो, आयोमा तथा नोगी आदि जापानी सेनापतियों को युद्धों का बहुत अनुभव था। अत: उन्होंने जापानी सेना का कुशल नेतृत्व किया। परिणामस्वरूप रूसी सेना जापानी सेना का मुकाबला न कर सकी एवं उसे पराजय का सामना करना पड़ा।
(5) रूस का ज़ार जापान की सैन्य शक्ति का ठीक अनुमान न लगा सका। वह यह ही समझता रहा कि युद्ध अथवा शांति का निर्णय उसी के हाथ में है। यह भ्रम ही रूस की पराजय तथा जापान की विजय का कारण बना।
(6) जापान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सदढ थी। वह इंग्लैंड की मित्रता पर भरोसा कर सकता था। परंत फ्राँस 1904 ई० के समझौते के कारण इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं लड़ सकता था। अतः रूस मित्रहीन था। अतः जापान ने आसानी से उसे पराजित कर दिया।
IV. रूस-जापान युद्ध के प्रभाव
रूस-जापान युद्ध के दूरगामी प्रभाव पड़े। संक्षेप में इसके प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. रूस पर प्रभाव (Effects on Russia)-रूस-जापान युद्ध से रूस की प्रतिष्ठा को गहरी चोट लगी। ज़ार शासकों के विरुद्ध पहले ही रूसी जनता में असंतोष व्याप्त था। ऊपर से जापान जैसे छोटे-से देश से पराजित होने पर लोग उनसे और नाराज हो गए। इस पराजय से जार शासकों की शक्ति का खोखलापन सारे विश्व के सामने आ गया तथा यूरोप के लोग इसकी आलोचना करने लगे।
2. जापान पर प्रभाव (Effects on Japan)-रूस-जापान युद्ध के जापान पर भी प्रभाव पड़े। इस युद्ध में विजय के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान का बहुत सम्मान बढ़ा। जापान एक छोटा-सा देश था फिर भी वह विशालकाय रूस पर विजय पाने में सफल रहा। इस विजय के कारण उसकी प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गए तथा दूर-पूर्व में उसका प्रभाव बढ़ गया।
इस विजय से जापान बहुत प्रोत्साहित हुआ। इस विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र है। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० यनागा के अनुसार,”इस प्रकार सुदूर पूर्व में एक नई शक्ति का उदय हुआ, एक छोटी पूर्वी शक्ति ने न केवल एक शक्तिशाली राष्ट्र को चुनौती प्रस्तुत की अपितु उसे कड़ी पराजय देने में भी सफलता प्राप्त की।
3. चीन पर प्रभाव (Effects on China)-रूस-जापान युद्ध के प्रभावों से चीन भी अछूता नहीं रहा। इस युद्ध के पश्चात् चीन के लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि यदि उन्होंने पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद से छुटकारा
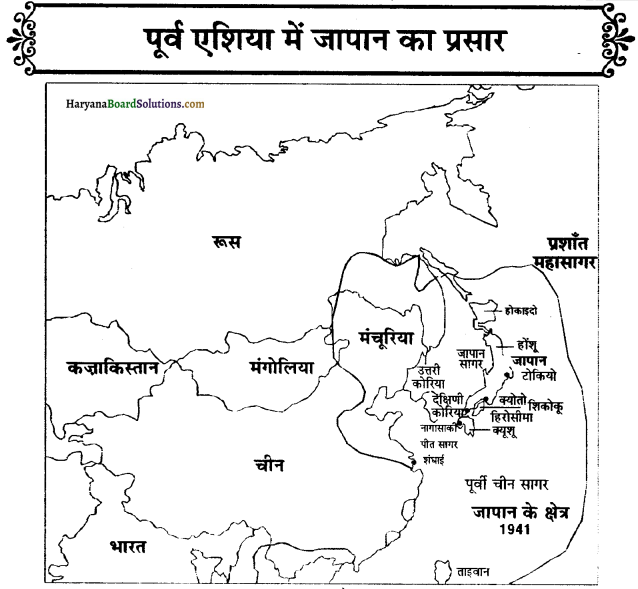
पाना है तो उन्हें अपनी शक्ति का पुनर्गठन करना होगा। अतः चीन ने अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए पश्चिमी युद्ध कला को अपनाया। पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने के लिए अनेक चीनी विदेशों में गए। अत: चीन के लोगों में एक नई जागृति का उत्थान हुआ। इसी राष्ट्रीय जागरण के परिणामस्वरूप चीन में 1911 ई० की क्रांति हुई और चीनी सम्राट् गद्दी छोड़ने पर विवश हुआ। इस प्रकार मांचू वंश का पतन हुआ तथा चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई।
4. यूरोप पर प्रभाव (Effects on Europe)-इस युद्ध के यूरोप की राजनीति पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े। युद्ध के समय जर्मनी ने रूस तथा फ्रॉस से मिल कर इंग्लैंड के विरुद्ध एक संगठन बनाने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल न हो सका। इसके विपरीत फ्रांस के प्रयत्नों से रूस और इंग्लैंड एक-दूसरे के निकट आए। इस युद्ध में रूस की पराजय से इंग्लैंड को रूस की ओर से कोई भय न रहा। इस कारण इंग्लैंड ने रूस की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया जिससे इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार एम० ई० कैमरन के अनुसार, “युद्ध में जापान की विजय के विश्व मामलों में गहन प्रभाव पड़े।”

प्रश्न 5.
जापान में सैन्यवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
जापान में सैन्यवाद के उदय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनमें से मुख्य कारणों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है
1. सैन्यवादियों की महत्त्वाकांक्षा:
जापान में सैन्यवादियों के उत्थान का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि वे जापान में फैली अशांति पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। 1894-95 में चीन-जापान युद्ध में तथा 1904-05 ई० में रूस-जापान युद्ध में जापान की सफलता ने विश्व को चकित कर दिया। 1902 ई० में जापान इंग्लैंड के साथ एक समझौता करने में सफल रहा। इन कारणों से जापान की सेना की महत्त्वाकांक्षा बढ़ गई। 1931 ई० में जापानी सेना ने सरकार से परामर्श किए बिना ही मंचूरिया पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया।
2. उदारवादियों की मृत्यु :
बहुत-से पुराने नेता सैन्यवादियों की गतिविधियों को पसंद . नहीं करते थे। वास्तव में वे सैन्यवादियों पर अंकुश रखते थे। परंतु ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया वे बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण सैन्यवादियों पर जो उनका अंकुश था वह समाप्त हो गया और वे अब अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो गये। दूसरे क्षेत्रों को विजय करने की उनकी इच्छा को अब कोई नहीं दबा सकता था।
3. नवयुवक अधिकारियों की श्रेणी का उदय:
जापान में नवयुवक अधिकारियों की एक नई श्रेणी का उदय हुआ। इन लोगों का संबंध जापान की कुलीन श्रेणी से नहीं था। यहाँ यह बात याद रखने योग्य है कि कुलीन श्रेणी के लोग इन नवयुवक लोगों को केवल पसंद ही नहीं करते थे बल्कि घृणा भी करते थे। उधर ये नवयुवक अधिकारी अपनी शानदार विजयों द्वारा समाज में अपना स्थान बनाना चाहते थे। उन्हें सैनिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था। वे जापानी सैनिकवाद में विश्वास करते थे और शक्ति का प्रयोग करना अपना अधिकार समझते थे।
4. नाजीवाद तथा फासिस्टवाद का प्रभाव:
हिटलर तथा मुसोलिनी की सफलताओं का जापानियों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अत: जापानी भी हिटलर तथा मुसोलिनी की भाँति विजयें प्राप्त करना चाहते थे। वे उनके विचारों तथा तरीकों से बहुत प्रभावित थे। विजयों की आकांक्षा रखने वाले जापानी नवयवक नाजी एवं फासिस्ट लोगों की तरह अपनी दशा को सधारना चाहते थे।
5. विरोधी नेता:
जापानी संसद् के सदस्य, उच्च अधिकारी तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्य सैन्यवादियों के घोर विरोधी थे। अपने इस विरोध के कारण ही वे सैन्यवादियों के आतंक का निशाना बने। जापान में सैन्यवादियों का विरोध करने वालों में शिक्षक तथा पत्रकार भी शामिल थे। वे भली-भाँति समझते थे कि सैनिक खर्च में वद्धि का क्या परिणाम होगा। जापान में उस समय सरकारी आमदनी सीमित तथा खर्चे असीमित थे।
देश पर पहले ही ऋण का भारी बोझ था। अतः एक के बाद एक वित्तमंत्री ने सैनिक खर्चों में कटौती करने के सझाव रखे। जापानी सेना इसलिए तैयार नहीं थी। अतः उसने विरोधियों को अपना निशाना बनाया।
6. उच्च-पदाधिकारियों का वध:
1937 ई० तक जापान में उग्र राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका था। सैन्यवादियों ने उग्र-राष्ट्रवाद का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया। पहले उन्होंने लोगों को डराया धमकाया और जब इससे काम न चला तो सैन्यवादियों ने उनका वध कर दिया। मंत्री, उच्च-पदाधिकारी, संसद् के सदस्य, पत्रकार तथा शिक्षक जो सैन्यवादियों के विरोधी थे, उन्हें पहले धमकी दी गई और जब उन्होंने इस पर भी सैन्यवादियों का विरोध करना न छोड़ा तो उनका वध कर दिया गया। इसने स्थिति को विस्फोटक बना दिया।
प्रश्न 6.
जापान पर अमरीका के कब्जे (1945-51 ई० ) के दौरान वहाँ क्या प्रगति हुई ? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
उत्तर:
जापान पर 1945 ई० से लेकर 1952 ई० तक अमरीका के जनरल दगलस मेकार्थर (General Douglas Mac Arthur) का शासन रहा। इसका उद्देश्य जापान का निशस्त्रीकरण करना, युद्ध अपराधियों पर अभियोग चलाना, जापान में एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना, जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं शिक्षा को एक नई दिशा देना था।
वह अपने उद्देश्य में काफी सीमा तक सफल रहा। इसके परिणामस्वरूप जापान पुनः एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। आज जापान की गणना विश्व के प्रसिद्ध देशों में की जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी० वी० राव के शब्दों में, “विश्व युद्ध के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने जापान पर कब्जे के पश्चात् महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। ये मेज़ी काल से कहीं अधिक क्रांतिकारी थे।”
1. जापान का निरस्त्रीकरण करना :
जनरल दगलस मेकार्थर ने सर्वप्रथम अपना ध्यान जापान को निरस्त्रीकरण करने की ओर दिया। इस कार्य के लिए उसने बहुत साहस से कार्य किया। उसने जापान की थल सेना एवं नौसेना को भंग कर दिया। उनके सभी हथियारों को नष्ट कर दिया। जापान में अनिवार्य सैनिक शिक्षा एवं सेवा को बंद कर दिया गया।
युद्ध सामग्री बनाने वाले सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया। उन्हें असैनिक सामान का उत्पादन करने का आदेश दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा युद्ध सामग्री की नई खोजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। जिन जापानी अधिकारियों ने जापान के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया था उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया। इस प्रकार जापान का निरस्त्रीकरण जापान में एक लंबे समय के पश्चात् एक स्थायी शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ।
2. युद्ध अपराधियों पर अभियोग :
जापान के जो अधिकारी युद्ध के लिए जिम्मेवार थे उन पर मुकद्दमा चलाया गया। इसके लिए तोक्यो में 1946 ई० में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत का गठन किया गया। इसने जापान के जनरल तोजो एवं कुछ अन्य अधिकारियों को मृत्यु दंड दिया। अनेक सैनिकों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जापान की पिछली सरकार द्वारा जितने उदार राजनीतिज्ञों को कारावास में डाल दिया गया था उन्हें रिहा कर दिया गया।
उग्र राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को सरकारी पदों से हटा दिया गया। इसी प्रकार उग्र राष्टीय विचारधारा वाले अध्यापकों को भी हटा दिया गया। इस विचारधारा का समर्थन करने वाली समितियों को भंग कर दिया गया एवं पाठ्यक्रम से ऐसी पुस्तकों को हटा दिया गया।
3. जापान का नया संविधान :
जापान में 1947 ई० में एक नया विधान लाग किया गया। इसने 1889 ई० के मेज़ी काल में प्रचलित संविधान का स्थान ले लिया। इस संविधान के अनुसार सम्राट् से उसकी अनेक शक्तियाँ छीन ली गईं। उसे अब देवता नहीं माना जाता था। अब जापान की डायट के अधिकार बढ़ा दिए गए। इसे अब देश के कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया।
नागरिक के अधिकारों में वृद्धि की गई। जापान को एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया गया। निस्संदेह जापान का नया संविधान लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में एक मील पत्थर सिद्ध हुआ।
4. आर्थिक सुधार :
द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जापान की अर्थव्यवस्था को भारी आघात लगा था। अत: जनरल दगलस मेकार्थर ने इस दिशा की ओर अपना विशेष ध्यान दिया। 1946 ई० में जापान की डायट द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसके अनुसार अनुपस्थित ज़मींदारों (absentee landlords) को अपनी भूमि सरकार को बेचने के लिए बाध्य किया गया। सरकार ने इन जमीनों को किसानों में बाँट दिया। इससे उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 1946 ई० में मजदूरों को श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार दिया गया।
उनकी दशा सुधारने के उद्देश्य से उनके वेतन, कार्य के समय, बेकारी भत्ते एवं बुढ़ापे के बीमे आदि की व्यवस्था की गई। जायबात्सु पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका कारण यह था कि देश की लगभग समस्त संपत्ति उनके हाथों में एकत्र हो गई थी। सरकार ने उन्हें उनके विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। अमरीका ने जापान में भारी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन सुधारों के चलते जापान की अर्थव्यवस्था पुनः पटड़ी पर आ गई।
5. शिक्षा सुधार :
आधिपत्यकाल में जापान में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए। जापान की परंपरावादी (traditional) शिक्षा को परिवर्तित कर दिया गया। जापान में पश्चिम में प्रचलित आधुनिक शिक्षा को लागू किया गया। पाठ्य पुस्तकों को नए ढंग से लिखा गया। इसमें सम्राट् की उपासना, नैतिक एवं सैनिक शिक्षा की अपेक्षा लोकतंत्र पर अधिक बल दिया गया था।
शिक्षण संस्थाओं में जापान में प्रचलित शिंटो धर्म के पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रबंध किया गया। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान ने विभिन्न क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की।
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एस० एन० सेन का यह कहना ठीक है कि, “जापान पर (अमरीका का) आधिपत्य यद्यपि 7 वर्ष तक रहा किंतु यह जापान के भावी विकास के लिए निर्णायक था।
प्रश्न 7.
1839-42 ई० के प्रथम अफ़ीम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ?
अथवा
प्रथम अफ़ीम युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
1839-42 ई० में इंग्लैंड एवं चीन के मध्य प्रथम अफ़ीम युद्ध हुआ। इस युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों, घटनाओं एवं प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
I. प्रथम अफ़ीम युद्ध के कारण
(Causes of the First Opium War) चीन तथा ब्रिटेन के मध्य प्रथम अफ़ीम युद्ध नवंबर, 1839 ई० में आरंभ हुआ था। यह युद्ध 1842 ई० तक चला। निस्संदेह अफ़ीम का व्यापार ही इस युद्ध का मुख्य कारण था परंतु इसके अन्य भी अनेक कारण थे । इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. चीन एवं ब्रिटेन के तनावपूर्ण संबंध:
विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक होने के कारण चीन निवासी अपनी उच्च सभ्यता पर बहुत गर्व करते थे। वहाँ के लोग पश्चिमी देशों के लोगों को निम्न मानते थे तथा उनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहते थे। चीन सरकार के अफसर तथा कर्मचारी यरोपीय व्यापारियों के साथ बहत अभद्र व्यवहार करते थे तथा उन्हें अपमानजनक चीनी कों का पालन करने के लिए विवश किया जाता था। अंग्रेज़ इन अपमानजनक एवं घटिया नियमों को को तैयार नहीं थे। अत: चीन तथा ब्रिटेन के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसने चीन एवं ब्रिटेन के मध्य होने वाले प्रथम अफ़ीम युद्ध को अनिवार्य बना दिया।
2. चीन में यूरोपीय व्यापारियों का शोषण:
यूरोपीय व्यापारी चीन से जो भी माल खरीदते थे उस पर लिए जाने वाले कर की दर सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई थी। चीनी सरकार के भ्रष्ट अधिकारी उनसे मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे जिस कारण यूरोपीय व्यापारी बहुत परेशान थे। चीन सरकार द्वारा स्थापित को-होंग (Co-Hong) नामक संस्था भी प्रायः विदेशी व्यापारियों का शोषण करती थी। चीन का सारा व्यापार को-होंग के माध्यम से ही होता था। चीन में यूरोपीय व्यापारियों का यह शोषण भी अफ़ीम युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना।
3. विदेशियों पर कठोर प्रतिबंध:
चीनी सरकार ने विदेशियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा रखे थे। विदेशी चीनी भाषा नहीं सीख सकते थे, चीनी नागरिक को दास नहीं रख सकते थे तथा न ही किसी चीनी नागरिक को अपने धर्म में दीक्षित कर सकते थे। विदेशी व्यापारी केवल व्यापार के लिए ही कैंटन में निवास कर सकते थे। इसके पश्चात् उन्हें मकाओ वापस जाना पड़ता था। वे कैंटन में अपने परिवार भी साथ नहीं ला सकते थे।
विदेशी अपनी फैक्टरियों में केवल निश्चित संख्या में ही चीनी नौकर रख सकते थे। वे चीन के आंतरिक भागों में नहीं जा सकते थे। इस कारण अंग्रेज़ चीन से अपमानजनक व्यवहार का बदला लेना चाहते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सी० ए० बस के अनुसार, “कैंटन में पूर्व एवं पश्चिम के मिलन ने गहरे मतभेदों को जन्म दिया जो कि युद्ध की ओर ले गए।”
4. अफ़ीम व्यापार (The Opium Trade)-अंग्रेज़ों ने 1767 ई० में चीन के साथ अफ़ीम का व्यापार आरंभ किया था। शीघ्र ही चीन में इसकी माँग बहुत बढ़ गई। चीन की सरकार ने अफ़ीम के व्यापार पर कई प्रतिबंध लगाए परंतु इसका कोई परिणाम न निकला। अब तक चीन के लोग अफ़ीम के आदी हो चुके थे तथा अंग्रेजों को इसका बहुत लाभ पहुँच रहा था।
चीन सरकार के भ्रष्ट अधिकारी भी भारी घूस लेकर इस व्यापार को प्रोत्साहन दे रहे थे। परिणामस्वरूप चीन में अफ़ीम की तस्करी में भारी वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 1837 ई० तक चीन के व्यापार में केवल अफ़ीम का आयात ही 57% तक हो गया था। चीन की सरकार इसे सहन करने को तैयार नहीं थी। अतः युद्ध के लिए विस्फोट तैयार था।
5. तात्कालिक कारण:
7 जुलाई, 1839 ई० को एक ऐसी घटना घटी जो प्रथम अफ़ीम युद्ध का तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। कुछ शराबी अंग्रेज़ नाविकों ने एक चीनी नाविक की हत्या कर दी। कैप्टन इलियट (Capt. Elliot) ने इन अंग्रेज़ नाविकों पर मुकद्दमा चलाकर उन्हें सजा दे दी तथा इस संबंधी चीनी सरकार को सूचित कर दिया। चीन की सरकार ने अपराधियों को उसे सौंपने के लिए कहा।
वह उन्हें अपने देश के कानूनों के अनुसार दंड देना चाहती थी। कैप्टन इलियट ने अपराधियों को सौंपने से इंकार कर दिया। इस बात पर कमिश्नर लिन ने अंग्रेजों को भेजी जाने वाली भोजन सामग्री तथा तेल की सप्लाई बंद कर दी। इसने प्रथम अफ़ीम युद्ध का बिगुल बजा दिया।
II. प्रथम अफ़ीम युद्ध की घटनाएँ
अंग्रेज़ सैनिकों तथा चीनी सैनिकों के मध्य प्रथम मुठभेड़ 3 नवंबर, 1839 ई० को हुई जिसमें ब्रिटिश सेनाओं ने चीन के तीन युद्धपोत नष्ट कर दिए। चीन की सरकार ने जनवरी, 1840 ई० को ब्रिटेन के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। उधर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन (Palmerston) भी चीन में अंग्रेज़ व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करने के पक्ष में था। इसी उद्देश्य से उसने अप्रैल, 1840 ई० में ब्रिटेन की संसद् में चीन के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पास करवा लिया। यह युद्ध लगभग दो वर्ष (1840-42 ई०) तक चला।
अंग्रेजों की संगठित तथा श्रेष्ठ सेना का मुकाबला चीनी सैनिक न कर सके। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कैंटन (Canton), निंगपो (Ningpo), अमोय (Amoy) तथा हांगकांग (Hong Kong) पर अधिकार कर लिया। 1842 ई० में अंग्रेजों ने शंघाई (Shangai) पर भी अधिकार कर लिया तथा नानकिंग की ओर बढ़ने लगे। विवश होकर चीनी सम्राट ने अंग्रेजों के साथ बातचीत करने का आदेश दिया। इस बातचीत के परिणामस्वरूप 29 अगस्त, 1842 ई० को दोनों देशों के मध्य नानकिंग की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया।
1. नानकिंग की संधि (Treaty of Nanking)-29 अगस्त, 1842 ई० को अंग्रेजों तथा चीनियों के बीच एक संधि हुई जो नानकिंग की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि की शर्ते निम्नलिखित थी
(1) हांगकांग का द्वीप सदा के लिए ब्रिटेन को सौंप दिया गया।
(2) ब्रिटिश लोगों को पाँच बंदरगाहों-कैंटन, अमोय, फूचाओ (Foochow), निंगपो और शंघाई में बसने तथा व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया।
(3) क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने दो करोड़ दस लाख डालर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया।
(4) को-होंग को भंग कर दिया गया। परिणामस्वरूप अब ब्रिटिश व्यापारी किसी भी चीनी व्यापारी के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था।
(5) आयात और निर्यात पर एक समान तथा उदार दर स्वीकार कर ली गई। (vi) चीनियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजों के मुकद्दमे अंग्रेज़ी कानून के अनुसार तथा उन्हीं की अदालतों में चलेंगे।
(6) यह भी शर्त रखी गई कि चीन अन्य देशों के लोगों को जो भी सुविधाएँ देगा वे अंग्रेजों को भी प्राप्त होंगी। एक अन्य इतिहासकार सी० ए० बस के शब्दों में, “यह एक युग का अंत एवं दूसरे युग का आगमन था।”
III. प्रथम अफ़ीम युद्ध के प्रभाव
प्रथम अफ़ीम युद्ध के परिणाम चीन के लिए बहुत ही विनाशकारी प्रमाणित हुए। इस युद्ध के परिणामों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. चीन की आर्थिक समस्याओं का बढ़ना:
प्रथम अफ़ीम युद्ध का सर्वप्रथम परिणाम यह हुआ कि चीन का आर्थिक शोषण आरंभ हो गया। अंग्रेज़ अब स्वतंत्रतापूर्वक अफ़ीम का व्यापार करने लगे। इस व्यापार के कारण चीन के धन का निकास होने लगा तथा चीन की आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गईं।
2. चीन के सम्मान को धक्का:
प्रथम अफ़ीम युद्ध के पश्चात् हुई नानकिंग की संधि के कारण चीन के सम्मान में लगातार कमी होने लगी। उसकी व्यापारिक श्रेष्ठता तथ का महत्त्व कम होने के कारण विदेशियों ने चीनी सरकार पर अपना दबाव बढाना आरंभ कर दिया। परिणामस्वरूप उन्होंने चीन से अनेक सुविधाएँ प्राप्त की। इससे चीन के सम्मान को गहरा आघात लगा।
3. खुले द्वार की नीति :
एक लंबे समय से चीन के द्वार विदेशी व्यापारियों के लिए बंद थे। विदेशी व्यापारियों को कैंटन के अतिरिक्त किसी और नगर में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। विदेशी व्यापारी सीधे चीनी व्यापारियों के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। वे केवल को-होंग के माध्यम से ही अपना व्यापार कर सकते थे। परंतु इस युद्ध के पश्चात् चीन की सरकार को खुले द्वार की नीति अपनानी पड़ी। इस नीति के कारण चीन की बहुत आर्थिक हानि हुई।
4. साम्राज्यवाद का युग :
चीनी लोग यूरोपीयों से बहुत पिछड़े थे। उनकी सैनिक शक्ति भी संगठित नहीं थी। इस स्थिति का लाभ उठा कर यूरोपीयों ने चीन की सरकार पर दबाव डाला तथा अपने लिए अनेक सुविधाएँ प्राप्त कर ली। धीरे-धीरे यूरोपियों ने चीन के तटवर्ती नगरों में अपने कारखाने स्थापित कर लिए और सेना भी रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने कुछ नगरों पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इससे साम्राज्यवाद का उदय हुआ तथा चीन पराधीन होने लगा।
5. ताइपिंग विद्रोह :
प्रथम अफ़ीम युद्ध में हुई चीन की पराजय तथा नानकिंग की संधि से माँचू शासन की दुर्बलता प्रकट हो गई। इस कारण चीन के विभिन्न भागों के लोग माँचू शासन के विरुद्ध हो गए। उन्होंने समय-समय पर कई विद्रोह कर दिए। इन विद्रोहों में से ताइपिंग विद्रोह सबसे प्रसिद्ध था। इस विद्रोह ने 1850 ई० से 1864 ई० के समय के दौरान चीन के कई भागों को अपनी चपेट में ले लिया। विद्रोहियों का उद्देश्य माँचू शासन को समाप्त करके मिंग वंश का शासन पुनः स्थापित करना था। यद्यपि इस विद्रोह का दमन कर दिया गया तथापि चीन के इतिहास में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है।

प्रश्न 8.
द्वितीय अफ़ीम युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अथवा
द्वितीय अफ़ीम युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले ?
उत्तर:
I. द्वितीय अफ़ीम युद्ध के कारण
द्वितीय अफ़ीम युद्ध चीन तथा ब्रिटेन के मध्य 1856-60 ई० में लड़ा गया। इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन अग्रलिखित अनुसार है
1. अफ़ीम के व्यापार में वृद्धि :
प्रथम अफ़ीम युद्ध का मुख्य कारण अफ़ीम का अवैध व्यापार था परंतु इस युद्ध के पश्चात् हुई संधियों में इसके व्यापार संबंधी कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ था। अंग्रेज़ अब भी धड़ल्ले से इसका व्यापार कर रहे थे। वे अफ़ीम के व्यापार से काफी लाभ कमा रहे थे। परिणामस्वरूप भारी मात्रा में अफ़ीम चीन में आने लगी।
1842 ई० में चीन में आने वाली पेटियों की संख्या 38,000 थी जोकि 1850 ई० तक 52,000 हो गई थी। चीन की सरकार इस अवैध व्यापार से बहुत चिंतित थी परंतु इस मामले में विदेशियों पर कोई ठोस प्रतिबंध लगाने में असमर्थ थी। इस प्रकार अफ़ीम का व्यापार द्वितीय अफ़ीम युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना।
2. चीनियों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार:
नानकिंग की संधि के पश्चात् विदेशियों ने अपने व्यापार का विस्तार करना आरंभ कर दिया। उन्हें यूरोप में कुलियों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने चीन के निर्धन युवकों को धन का लालच देकर यूरोप के देशों तथा संयुक्त राज्य अमरीका आदि में भेजना आरंभ कर दिया। विदेशों में इन चीनियों से दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। चीन की सरकार विदेशों में चीनियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को सहन करने को तैयार नहीं थी। इस कारण चीन तथा यूरोपियों के संबंध तनावपूर्ण हो गए।
3. अधिकारों का दुरुपयोग:
प्रथम अफ़ीम युद्ध के पश्चात् 8 अक्तूबर, 1843 ई० को हुई बोग की संधि (Treaty of Bogue) के अनुसार अंग्रेजों ने चीन में अपने देश के कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। परंतु चीन की सरकार की दुर्बलता का लाभ उठा कर वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे थे। चीन की सरकार इसे सहन करने को तैयार नहीं थी।
4. कैथोलिक प्रचारक की हत्या :
आगस्ते चैप्डेलेन (Auguste Chapdelaine) नामक कैथोलिक प्रचारक की हत्या भी द्वितीय अफ़ीम युद्ध का एक मुख्य कारण सिद्ध हुई। चैप्डेलेन फ्राँस का निवासी था। वह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए चीन में आया था। वह अपने धर्म-प्रचार के प्रयास में चीन के आंतरिक भागों में काफी दूर तक चला गया। चीन के अधिकारियों ने इसे संधि की शर्तों का उल्लंघन माना तथा उसे बंदी बना लिया।
उस पर चीनी सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। क्वांगसी की स्थानीय अदालत ने फरवरी 1856 ई० में उसे मृत्यु दंड दे दिया। चीनी सरकार के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर नेपोलियन तृतीय ने चीन के विरुद्ध युद्ध में इंग्लैंड को साथ देने का मन बना लिया।
5. तात्कालिक कारण :
1856 ई० में घटने वाली लोर्चा ऐरो घटना (Lorcha Arrow Incident) द्वितीय अफ़ीम युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। 8 अक्तूबर, 1856 ई० को चीनी अधिकारियों ने लोर्चा ऐरो नामक जहाज़ को पकड़ लिया तथा उसके 14 में से 12 नाविकों को बंदी बना लिया। इन पर यह इल्जाम लगाया कि वे प्रतिबंधित अफ़ीम का व्यापार कर रहे हैं। यह जहाज़ एक चीनी व्यापारी का था किंतु इसका कप्तान एक अंग्रेज़ था।
इस जहाज़ पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था। अंग्रेजों ने चीन की इस कार्यवाही की निंदा की तथा बंदी बनाए गए व्यक्तियों को छोड़ने तथा उचित मुआवजा देने के लिए कहा। चीनी अधिकारियों ने अपनी कार्यवाही को उचित ठहराया तथा अंग्रेजों की माँग मानने से इंकार कर दिया। चीनियों के इस व्यवहार से अंग्रेज रुष्ट हो गए तथा उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार इमानूएल सी० वाई० सू के शब्दों में, “1856 ई० की लोर्चा ऐरो घटना ने ब्रिटेन को अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया।”
II. द्वितीय अफ़ीम युद्ध की घटनाएँ
1856 ई० में अंग्रेज सेनाओं ने कैंटन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् फ्रांसीसी सेनाएँ भी ब्रिटिश सेनाओं की सहायता के लिए पहुंच गई । शीघ्र ही दोनों सेनाएँ तीनस्तीन पहुँच गईं। चीनी सरकार इस संयुक्त सेना का सामना करने में असमर्थ थी। अतः परिणामस्वरूप चीनियों ने बाध्य होकर इन देशों के साथ 26 जून, 1858 ई० को तीनस्तीन की संधि कर ली।
1. तीनस्तीन की संधि 1858 ई० (Treaty of Tientsin 1858 CE)-तीनस्तीन की संधि पर 26 जून, 1858 ई० को चीन, इंग्लैंड तथा फ्राँस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थीं
(1) चीन की 11 नई बंदरगाहों को विदेशी देशों के साथ व्यापार तथा निवास के लिए खोल दिया गया।
(2) चीनी सरकार ने पश्चिमी देशों को अफ़ीम के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी तथा अफ़ीम के व्यापार को वैध घोषित कर दिया।
(3) चीन की ‘यांगत्सी’ नदी में पश्चिमी देशों के जहाजों को आने-जाने की अनुमति दे दी गई।
(4) चीन की सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया कि पश्चिमी देश चीन में अपने राजदूत नियुक्त कर सकेंगे।
(5) चीन की सरकार ने फ्रांस के रोमन कैथोलिक पादरियों को यह सुविधा प्रदान कर दी कि वे उपर्युक्त सोलह बंदरगाहों को छोड़कर कहीं भी आ-जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे किसी भी स्थान पर भूमि खरीद सकते हैं अथवा किराये पर भूमि लेकर गिरजाघरों का निर्माण कर सकते हैं।
(6) ईसाई धर्म के प्रचारकों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे चीन में स्वतंत्रतापूर्वक घूम-फ़िर कर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल ईसाई बना सकते हैं।
(7) पश्चिमी शक्तियों के राज्य-क्षेत्रातीत अधिकारों (Extra Territorial Rights) को अधिक विस्तृत और व्यापक कर दिया गया। इसके अनुसार उन्हें चीन में निवास करने और व्यापार करने की सुविधा दी गई।
(8) चीन ने अंग्रेज़ व्यापारियों को युद्ध के हर्जाने के रूप में एक भारी धन-राशि देना स्वीकार कर लिया।
(9) इस संधि ने उन विदेशियों को जिनके पास वैध प्रवेश पत्र (legal passport) हों, चीन के किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक घूमने-फिरने की अनुमति प्रदान कर दी।
2. युद्ध का दूसरा चरण:
26 जून, 1858 ई० को तीनस्तीन की संधि हो गई थी प चीन की सरकार ने इसे मान्यता देने से इंकार कर दिया था। चीन की इस कार्यवाही से पश्चिमी शक्तियों को बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने चीनी सरकार पर दबाव डालने के लिए पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने शीघ्र ही पीकिंग पर आक्रमण कर दिया।
चीन की निर्बल सेना इस आक्रमण का मुकाबला करने में नाकाम रही। संयुक्त सेनाओं ने पीकिंग पर अधिकार कर लिया तथा माँचू सम्राट् पीकिंग छोड़ कर भाग गया। विजयी सेनाओं ने नगर में भारी लूट-मार की तथा राजमहल को अग्नि भेंट कर दिया। विवश होकर चीन की सरकार को पीकिंग की संधि की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। पीकिंग की संधि 1860 ई० (Treaty of Peking 1860 CE)-अक्तूबर, 1860 ई० में चीन, फ्राँस तथा इंग्लैंड के मध्य की गई पीकिंग संधि की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं
(1) अफ़ीम के व्यापार को वैध मान लिया गया।
(2) चीन सरकार ने पहले केवल 5 बंदरगाहें ही विदेशी व्यापार के लिए खोली थीं। अब 11 अन्य बंदरगाहें भी खोल दी जिससे बंदरगाहों की कुल संख्या 16 हो गई।
(3) चीन की सरकार पीकिंग में अंग्रेज़ राजदूत रखने के लिए मान गई।
(4) कौलून का प्रायद्वीप इंग्लैंड को दिया गया।
(5) चीन की सरकार को युद्ध के हर्जाने के रूप में आठ-आठ मिलियन डालर इंग्लैंड तथा फ्रांस को देने पड़े।
(6) चीन ने यह भी माना कि कैथोलिक पादरियों को 16 बंदरगाहों के अतिरिक्त चीन के किसी भी भाग में जाने की अनुमति होगी। उन्हें वहाँ धर्म प्रचार करने, भूमि खरीदने तथा गिरजाघर बनाने का अधिकार होगा।
II. द्वितीय अफ़ीम युद्ध के प्रभाव
द्वितीय अफ़ीम युद्ध के पश्चात् पूर्व के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युद्ध के प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. चीन के सम्मान को धक्का :
चीन निवासी सदियों से स्वयं को पश्चिमी लोगों से सभ्य मानते थे। उन्हें अपनी सभ्यता पर बहुत गर्व था। द्वितीय अफ़ीम युद्ध में पराजित होने के कारण चीनियों को अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े तथा विदेशियों को अपने से श्रेष्ठ मानना पड़ा। इस प्रकार उनके सम्मान को गहरा धक्का लगा।
2. चीन को आर्थिक हानि :
चीन लगभग चार वर्ष तक युद्धों में उलझा रहा। इन युद्धों में उसे भारी धन राशि खर्च करनी पड़ी। द्वितीय अफ़ीम युद्ध के दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस की सेनाओं ने चीन की राजधानी पीकिंग तथा अन्य नगरों में सरकारी संपत्ति को बहुत हानि पहुँचाई। इस युद्ध के पश्चात् हुई संधियों के अनुसार चीन को भारी धन राशि विजयी देशों को देनी पड़ी। इससे चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई।
3. ईसाई मत का प्रसार :
द्वितीय अफ़ीम युद्ध के पश्चात् हुई पीकिंग की संधि के अनुसार अब कैथोलिक पादरियों को 16 बंदरगाहों के साथ-साथ चीन के आंतरिक भागों में जाने तथा प्रचार करने की अनुमति मिल गई। परिणामस्वरूप ये पादरी चीन के विभिन्न भागों में बेरोक-टोक ईसाई मत का प्रचार करने लगे। उनके प्रचार से प्रभावित होकर अनेक चीनी नागरिकों ने ईसाई मत ग्रहण कर लिया।
इस कारण उनके धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन ईसाइयों की गतिविधियाँ ही चीन में 1899-1900 ई० में हुए बॉक्सर विद्रोह का कारण बनीं।
4. साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन :
द्वितीय अफ़ीम युद्ध से पूर्व यूरोपीय शक्तियों का उद्देश्य केवल चीन की बंदरगाहों पर अधिकार जमाना तथा व्यापार को संचालित करना था। इस युद्ध में विजयी रहने पर उन्हें 16 बंदरगाहों पर व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए। अब उन्होंने चीन में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। अब इन शक्तियों ने अपनी बस्तियाँ बसानी आरंभ कर दी तथा कई नगरों में अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इस प्रकार उन्होंने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया।
प्रश्न 9.
चीन के इतिहास में डॉक्टर सन-यात-सेन की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर-चीन के इतिहास में डॉ० सन-यात-सेन (1866-1925 ई०) का एक विशेष स्थान है। उन्हें आधुनिक न का निर्माता कहा जाता है। वह चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गणतंत्र की स्थापना उनके जीवन का परम लक्ष्य था।
1. प्रारंभिकजीवन :
डॉ० सन-यात-सेन का जन्म 2 नवंबर, 1866 ई० को कुआंगतुंग (Kwangtung) प्रदेश के चोय-हंग (Choy-Hung) नामक एक छोटे से गाँव में हुआ था। यह गाँव कैंटन (Canton) नगर से 40 मील की दूरी पर स्थित है। इनके पिता का नाम सन-टैट-सुंग (Sun-Tat-Sung) था। डॉ० सन-यात-सेन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए हवाई द्वीप (Hawaii Islands) में भेजा गया। उनके भाई ने डॉ० सन-यात-सेन को एंगलीकन चर्च के एक प्रसिद्ध स्कूल में भर्ती करा दिया।
इस स्कूल में उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। डॉ० सन-यात सेन ने लंदन में 1887 ई० में एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 1892 ई० में उन्होंने डॉक्टरी की परीक्षा पास की और मैकाय (Macoy) नामक स्थान पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस आरंभ कर दी। उस समय उनके ऊपर क्रांतिकारी भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ चुका था। वह देश की शिक्षा-प्रणाली में सुधार करना चाहते थे। उनका विचार था कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होने के पश्चात् ही देश उन्नति कर सकता है। वह चाहते थे कि माँचू सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करे।
2. रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना :
डॉ० सन यात-सेन ने 24 नवंबर, 1894 ई० को होनोलल (Honolulu) में रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की। वह स्वयं इस संस्था के चेयरमैन बने। इसे शिंग चुंग हुई (Hsing Chung Hui) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गुप्तचर संगठन था। आरंभ में इसके 112 सदस्य थे। 21 फरवरी, 1895 ई० को इसका मुख्यालय हांगकांग (Hong Kong) में खोला गया।
इसकी अनेक शाखाएँ चीन के विभिन्न प्रांतों में खोली गई। इसका प्रमुख उद्देश्य चीन में से माँचू शासन का अंत करना, चीनी समाज का पुनः निर्माण करना, प्रेस तथा शिक्षा के माध्यम से चीनियों में एक नवचेतना का संचार करना तथा चीन में गणतंत्र की स्थापना करना था।
3. तुंग मिंग हुई की स्थापना :
डॉ० सन-यात-सेन द्वारा 20 अगस्त, 1905 ई० को जापान की राजधानी तोक्यो (Tokyo) में तुंग मिंग हुई की स्थापना करना एक प्रशंसनीय कदम था। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य चीन में माँचू वंश का अंत करना, चीन को पश्चिमी देशों के शासन से मुक्त करना, चीन में लोकतंत्रीय गणतंत्र की स्थापना करना तथा भूमि का राष्ट्रीयकरण करना था। तुंग मिंग हुई की स्थापना वास्तव में चीन के इतिहास में एक मील पत्थर सिद्ध हुई।
4. डॉ० सन-यात-सेन के तीन सिद्धांत :
डॉ० सन-यात-सेन आरंभ से ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। वह लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। उन्होंने ही माँचू सरकार को हटा कर चीन में गणराज्य की स्थापना की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह रूसी साम्यवाद से बहुत प्रभावित थे, फिर भी वह रूसी विचारों का अंधा-धुंध अनुसरण नहीं करना चाहते थे। वह इस बात को भली-भाँति समझते थे कि रूस श्रमिकों का देश है और चीन किसानों का।
अत: उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। डॉ० सन-यात-सेन के राजनीतिक विचार तीन सिद्धांतों पर आधारित थे। ये सिद्धांत सन-मिन-चुई (San-min Chui) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
(1) राष्ट्रीयता:
डॉ० सन-यात-सेन राष्ट्रीयता के महत्त्व को भली-भाँति समझते थे। उनके विचारानुसार चीन को जिन वर्तमान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसका मूल कारण चीनी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है।
इसी कारण पश्चिमी देश चीन का घोर शोषण कर रहे हैं तथा जिस कारण वह विश्व का अग्रणी देश होने की अपेक्षा एक गरीब एवं कमज़ोर राष्ट्र बनकर रह गया है। अतः चीन की खुशहाली के लिए यह आवश्यक है कि चीनी लोगों में राष्ट्रवाद एवं देश-प्रेम की भावना का विकास हो। इसके लिए निम्नलिखित शर्ते आवश्यक थीं
- चीन से माँचू वंश का अंत करना।
- चीन को पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से मुक्त करना।
- चीनियों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना।
- विभिन्न समुदायों के लोगों में प्रचलित मतभेदों को दूर करना।
- चीन की स्वतंत्रता के लिए विदेशी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करना।
(2) राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy)-डॉ० सन-यात-सेन राजनीतिक लोकतंत्र को बहुमूल्य मानते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन विदेशों में व्यतीत किया था। अतः वह लोकतंत्र के महत्त्व से अच्छी तरह परिचित थे। यही कारण था कि वह चीन में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना के पक्ष में थे।
वह चाहते थे कि चीन में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हो किंतु यह सरकार अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसी सरकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को बिना किसी मतभेद के वोट डालने का अधिकार हो तथा वे अपनी सरकार को वापस बुलाने (recall) का अधिकार रखते हों।
(3) लोगों की आजीविका:
डॉ० सन-यात-सेन लोगों की आजीविका के महत्त्व को भली-भाँति समझते थे। यदि किसी देश के लोग भूखे हों तो उस देश का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। क्योंकि अधिकाँश चीनी कृषि, कार्य करते थे इसलिए उन्होंने इस ओर अपना विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ‘जोतने वाले को जमीन दो’ (land to the tiller) का नारा दिया।
चीन की आर्थिक खुशहाली के लिए उसके यातायात के साधनों, उद्योगों एवं खानों का विकास किया जाना चाहिए। इसके चलते मजदूरों को संपूर्ण रोजगार प्राप्त होगा तथा वे देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसके अतिरिक्त वह जमींदारों, व्यापारियों एवं पूँजीवादियों के हाथों में धन के केंद्रीयकरण (concentration of wealth) के विरुद्ध थे। वह सभी विशाल प्राइवेट उद्यमों (enterprises) का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण (nationalisation) के पक्ष में थे।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डॉ० सन-यात-सेन न केवल एक महान क्रांतिकारी थे अपितु आधुनिक चीन के निर्माता थे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से चीनी समाज को एक नई दिशा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। प्रसिद्ध इतिहासकार जी० डब्ल्यू० कीटन का यह कहना ठीक है कि,”डॉक्टर सन-यात-सेन ने 40 करोड़ चीनियों के लिए वही किया जो कमाल अतातुर्क ने तुर्की के लिए किया, जो लेनिन एवं स्टालिन ने रूस के लिए किया।”

प्रश्न 10.
1911 ई० की चीनी क्रांति के कारणों और उसके परिणामों का वर्णन कीजिएं।
अथवा
1911 ई० की चीनी क्रांति के क्या कारण थे?
उत्तर:
1. 1911 ई० की चीनी क्रांति के कारण थे
1. माँचुओं का पतन:
माँचू शासक मंचूरिया के रहने वाले थे। उन्होंने 1644 ई० में चीन में मिंग (Ming) वंश का अंत करके छींग (Qing) अथवा मांचू वंश की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की शान एवं शक्ति कम होने लगी। इसका कारण यह था कि माँचू शासक अब बहुत विलासी एवं भ्रष्ट हो चुके थे।
वे अब अपना अधिकाँश समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करने लगे थे। अतः उन्होंने प्रशासन की ओर अपना कोई ध्यान नहीं दिया। अतः प्रजा में बहुत असंतोष फैल गया था। मांचू शासकों द्वारा विदेशियों के साथ की जाने वाली अपमानजनक संधियों ने माँचू शासकों की निर्बलता को प्रकट कर दिया था। निस्संदेह चीनी इस अपमान को सहन करने को तैयार नहीं थे।
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के० टी० एस० सराओ का यह कहना ठीक है कि, “माँचू वंश के चक्र ने जिन्हें उन्हें अपनी गौरवता के शिखर पर पहुँचाया था वह अब उन्हें तीव्रता से उनके विनाश की ओर ले जा रहा था।”
2. चीन में सुधार आंदोलन :
1894-95 ई० में जापान ने चीन को पराजित कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। एशिया के एक छोटे-से देश से पराजित होना चीन के लिए एक घोर अपमान की बात थी। इसके पश्चात् चीन में रियायतों के लिए संघर्ष (Battle of Concessions) आरंभ हो गया था। इसने चीन की स्थिति को अधिक दयनीय बना दिया था।
चीन को इस घोर संकट से बाहर निकालने के लिए दो छींग सुधारकों कांग यूवेई (Kang Youwei) तथा लियांग किचाउ (Liang Qichao) ने चीनी सम्राट कुआंग शू (Kuang Hsu) को कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार लागू करने का सुझाव दिया। सम्राट् ने उनके सुझावों को मानते हुए 1898 ई० में सौ दिनों तक अनेक अध्यादेश जारी किए।
इन्हें चीनी इतिहास में सुधारों के सौ दिन (Hundred Days of Reforms) कहा जाता है। इनके अधीन चीन में एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, कानून व्यवस्था, राजस्व, रेलवे, डाक व्यवस्था, सेना एवं नौसेना, यातायात के साधनों के विकास, सिविल सर्विस में सुधार तथा संवैधानिक सरकार के गठन के बारे में उल्लेख किया गया।
यद्यपि ये सुधार बहुत प्रशंसनीय थे, किंतु इनको महारानी त्जु शी (Tzu Hsi) के विरोध के चलते लागू न किया जा सका। उसने बड़ी संख्या में सुधारकों को बंदी बना कर मौत के घाट उतार दिया। इससे चीनियों में व्यापक असंतोष फैला तथा उन्होंने ऐसे निकम्मे शासन का अंत करने का निर्णय किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जीन चैसनिआक्स का यह कहना ठीक है कि, “वे सुधार जो कि माँचू वंश द्वारा मुक्ति के साधन के तौर पर अपनाए गए थे उनके पतन का कारण बने थे।
3. त्जु शी की मृत्यु :
त्जु शी चीन की राजनीति में सबसे प्रभावशाली महारानी थी। उसने 1861 ई० से लेकर 1908 ई० तक चीन की राजनीति में अपनी गहरी छाप छोड़ी। वह बहुत रूढ़िवादी, अहंकारी एवं षड्यंत्रकारी महिला थी। उसने अपनी चतुर कूटनीति द्वारा माँचू वंश के पतन को रोके रखा। उसने 1898 ई० में सम्राट् कुआंग शू के सुधारों को रद्द कर दिया। उसने चीनी सुधारकों का निर्ममता से दमन कर दिया। 1908 ई० में त्जु शी की मृत्यु से माँचू वंश को एक गहरा आघात लगा।
4. शिक्षा का प्रसार :
शिक्षा के प्रसार ने चीन में 1911 ई० की क्रांति लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। चीन में शताब्दियों से प्राचीन शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। इस प्रणाली में केवल धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर बल दिया जाता था। 1902 ई० में चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय (Peking University) स्थापित किया गया।
1905 ई० में चीन में प्राचीन शिक्षा के अंत एवं आधुनिक शिक्षा को लागू करने की घोषणा की गई। निस्संदेह यह एक उल्लेखनीय कदम था। शिक्षा के प्रसार के कारण चीनी लोगों में एक नवचेतना का संचार, हुआ। अनेक चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों में गए। ये विद्यार्थी पश्चिम में हुए विकास को देख कर चकित रह गए। जब ये विद्यार्थी चीन वापस लौटे तो चीन की सरकार उन्हें योग्य नौकरियाँ देने में विफल रही। इस कारण इन विद्यार्थियों में चीनी सरकार के विरुद्ध घोर निराशा फैली। अत: उन्होंने ऐसी सरकार का अंत करने का निर्णय किया।
5. आर्थिक निराशा:
चीन की दयनीय आर्थिक दशा 1911 ई० की क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। प्रथम अफ़ीम युद्ध (1839-42 ई०) के पश्चात् यूरोपीय लुटेरों ने चीन का दरवाजा बलपूर्वक खोल दिया। उन्होंने चीन में लूट-खसूट का एक ऐसा दौर आरंभ किया जिस कारण वह कंगाली के कगार पर जा पहुँचा।
चीन की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया। खाद्यान्न की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हो गए। इस घोर संकट के समय प्रकृति ने भी चीन में अपना कहर ढाया। 1910-11 ई० में चीन भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया। इस कारण जन-धन की अपार हानि हुई।
इससे चीन की अर्थव्यवस्था को एक गहरा आघात लगा। ऐसे समय में चीन की सरकार ने लोगों पर भारी कर लगा कर एक भयंकर भूल की। अतः चीन के लोगों ने माँचू सरकार को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। एच० एम० विनायके के शब्दों में, “इसने लोगों में माँचू वंश के विरुद्ध बेचैनी एवं असंतुष्टता को और बढ़ा दिया। 120
6. प्रेस की भूमिका:
1911 ई० की चीनी क्रांति लाने में प्रेस ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। चीन में समाचार-पत्रों का प्रकाशन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आरंभ हुआ था। चीन में प्रकाशित होने वाले प्रारंभिक समाचार-पत्र अंग्रेजी भाषा में थे। 1870 ई० में चीनी भाषा में प्रथम समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् इन समाचार-पत्रों की संख्या तीव्रता से बढ़ने लगी। इन समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं ने माँचू सरकार के विरुद्ध लोगों में एक नवचेतना का संचार करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
7. डॉ० सन-यात-सेन का योगदान:
डॉ० सन-यात-सेन ने 1911 ई० की चीनी क्रांति में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस कारण उन्हें चीनी क्रांति का पिता कहा जाता है। वह इंग्लैंड, फ्राँस, अमरीका एवं जापान के हाथों से चीन की लगातार पराजयों से बहुत निराश हुए। इन पराजयों से चीन को घोर अपमान को सहन करना पड़ा। अत: डॉ० सन-यात-सेन ने चीन से अयोग्य माँचू सरकार का अंत करने का निर्णय लिया।
इस उद्देश्य से उन्होंने 1894 ई० में होनोलूलू में रिवाइव चाइना सोसायटी (Revive China Society) तथा 1905 ई० में तोक्यो में तुंग मिंग हुई (Tung Meng Hui) की स्थापना की। प्रसिद्ध इतिहासकार इमानुएल सी० वाई० सू का यह कहना ठीक है कि, “तुंग मिंग हुई की स्थापना चीनी क्रांति के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुई क्योंकि इसने क्रांति के स्वरूप एवं दिशा को परिवर्तित कर दिया था।”
वास्तव में डॉ० सन-यात-सेन ने चीनियों में एक नई जागृति लाने एवं उनमें एकता स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए। इस दिशा में उसके समाचार-पत्र मिन पाओ (Min Pao) ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। निस्संदेह 1911 ई० की चीनी क्रांति में डॉ० सन-यात-सेन ने जो प्रशंसनीय भूमिका निभाई उसके लिए उनका नाम चीनी इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
8. तात्कालिक कारण :
चीन की सरकार द्वारा रेलों का राष्ट्रीयकरण करना 1911 ई० की चीनी क्रांति का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। 1909 ई० में चीन की सरकार ने रेलमार्गों के निर्माण की एक विशाल योजना बनाई। यह कार्य प्रांतीय सरकारों को सौंपा गया। किंतु प्रांतीय सरकारें धन की कमी के कारण इन योजनाओं को संपूर्ण करने में विफल रहीं।
अतः मई 1911 ई० में चीनी सरकार ने रेलों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की। अत: रेलमार्गों के निर्माण का कार्य केंद्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ऐसा होने से प्रांतीय गवर्नर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध हो गए। वे क्रांतिकारयिों से मिल गए। उन्होंने 1911 ई० की चीनी क्रांति का बिगुल बजा दिया।
II. 1911 ई० की चीनी क्राँति की घटनाएँ।
10 अक्तूबर, 1911 ई० को हैंको में एक ऐसी घटना घटी जिसने क्राँति को तीव्र गति प्रदान कर दी। उस दिन हैंको में एक रूसी परिवार के घर एक बम-विस्फोट हुआ। यह घर क्रांतिकारियों का अड्डा था तथा वहाँ बमों का निर्माण किया जाता था। इस घटना के पश्चात् कई क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया तथा चीनी सरकार के हवाले कर दिया गया।
चीन की सरकार ने कुछ क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दे दिया। सरकार की इस दमन नीति से उत्तेजित होकर वूचांग के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही बहुत से ग्रामीण विद्रोही भी उनसे आ मिले। इन क्रांतिकारियों नेवू-तिंग-फंग के नेतृत्व में एक सैनिक सरकार का गठन किया तथा नानकिंग को अपनी राजधानी घोषित किया। उस समय डॉ० सन-यात-सेन अमरीका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था।
वह 24 दिसंबर, 1910 ई० को शंघाई पहुँचा और सभी क्रांतिकारियों ने उसे अपना नेता मान लिया। डॉ० सन-यात-सेन ने सुझाव दिया कि माँचू वंश का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की जाए। उसने गणतंत्र का राष्ट्रपति युआन-शी-काई को बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे युआन-शी-काई ने स्वीकार कर लिया। डॉ० सन-यात-सेन ने राजनीतिक संन्यास लेने का मन बना लिया।
परिणामस्वरूप 12 फ़रवरी, 1912 ई० को एक शाही घोषणा की गई जिसके अनुसार सारी राजनीतिक शक्ति युआन शी-काई को सौंप दी गई। 13 फ़रवरी को वह प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुआ और माँचू वंश का सदा के लिए अंत हो गया।
III.1911 ई० की चीनी क्रांति का महत्त्व
1911 ई० की क्रांति चीन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति से चीन में तानाशाही का अंत हुआ तथा गणतंत्र स्थापित हुआ। इस क्रांति के अनेक दूरगामी परिणाम निकले। प्रसिद्ध इतिहासकार के० टी० एस० सराओ ने ठीक लिखा है कि, “1911 ई० की चीन की क्रांति आधुनिक विश्व के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति ने एक युग का अंत किया एवं एक नए युग का सूत्रपात किया। 22
1. माँचू वंश का अंत :
1911 ई० की क्रांति का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि लगभग तीन सौ वर्षों से स्थापित माँचू शासन का अंत हो गया। माँचू शासक अयोग्य, भ्रष्ट तथा विलासी थे। न तो वे कुशल शासन प्रबंध दे सके तथा न ही विदेशी शक्तियों का सामना कर सके। वे अत्यंत रूढ़िवादी थे। चीन के लोग ऐसे शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। 1911-12 ई० में चीन के लोगों ने बिना कठिनाई तथा किसी का खून बहाए इस राजवंश का अंत कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन सेल्बी के अनुसार, “1912 ई० में कागजी ड्रेगन का अंत हो गया।”
2. राजतंत्र का अंत :
1911 ई० की क्रांति ने चीन में राजतंत्र का अंत कर दिया था। 1912 ई० में युआन-शी-काई (Yuan-Shih-Kai) चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना था। वह गणतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। वह राजतंत्र के पक्ष में था। 1915 ई० में उसने चीन में राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया किन्तु विफल रहा। 1916 ई० में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही चीन में राजतंत्रीय विचारधारा का भी अंत हो गया।
3. नए विचार:
1911 ई० की क्रांति के कारण चीन के शिक्षित नवयुवकों में नवीन विचारों का संचार हुआ। जो युवक पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त कर के आए वे नवीन विचारों से ओत-प्रोत थे । उन्होंने अपने देश में रूढ़िवादी सामाजिक ढाँचे को बदलने के प्रयास आरंभ कर दिए। अनेकों प्रसिद्ध पश्चिमी लेखकों के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। पश्चिमी विचारकों से प्रेरित होकर चीनी लोगों का दृष्टिकोण बदल गया।
4. माओ-त्सेतुंग का उत्थान:
1911 ई० की क्रांति के पश्चात् युआन शी-काई की गणतंत्रीय तथा चियांग-काई-शेक (Chiang-Kai-Shek) की राष्ट्रीय सरकारें बनीं। परंतु ये सरकारें भी देश को कठिनाइयों के भंवर से बाहर न निकाल सकीं। तब 1921 ई० में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। चियांग काई-शेक की सरकार साम्यवादी दल को समाप्त करना चाहती थी।
परंतु वह असफल रही। शनैः-शनैः साम्यवादी दल का प्रभाव गाँवों में भी बढ़ने लगा। साम्यवादियों ने चीन में 1934 ई० में एक लाँग मार्च (Long March) का आयोजन किया। इस मार्च में लगभग एक लाख लोगों ने भाग लिया। इसी मार्च के दौरान प्रसिद्ध नेता माओ-त्सेतुंग का उत्थान हुआ।
5. चीन का आधुनिकीकरण :
राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के पश्चात् चीन धीरे-धीरे आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ। देश में एक अस्थायी संविधान लागू किया गया। स्वास्थ्य, उद्योग, सिंचाई, संचार आदि से संबंधित कई सुधार किए गए। शिक्षा क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। मुद्रा संबंधी किए गए सुधारों से चीन में आर्थिक तथा व्यापारिक स्थिरता आई। राष्ट्रीय सरकार की विदेश नीति भी आर्थिक उत्थान में बड़ी सहायक सिद्ध हुई। निस्संदेह यह क्रांति चीन के इतिहास में एक नया मोड़ सिद्ध हुई।
प्रश्न 11.
कुओमीनतांग के उत्थान एवं सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
उत्तर:
कुओमीनतांग चीन का एक महत्त्वपूर्ण दल था। इस दल ने चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए बड़ा सराहनीय काम किया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस दल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी इस दल ने देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिये काफी कुछ किया। सच तो यह है कि इस दल का उत्थान चीन के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी।
1. कुओमीनतांग की स्थापना :
1905 ई० में डॉ० सन-यात-सेन ने जापान में तुंग-मिंग-हुई नामक दल की स्थापना की थी। आरंभ में यह संस्था एक गुप्त समिति के रूप में कार्य करती थी, परंतु 1911 ई० की चीनी क्रांति के समय यह दल काफी शक्तिशाली हो गया था। 1912 ई० में तुंग-मिंग-हुई तथा चीन के अन्य दलों को मिला कर एक नये राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। इस दल का नाम कुओमीनतांग रखा गया।
जब 1913 ई० में संसद् के चुनाव हुए तो इस दल को काफी सफलता प्राप्त हुई। यह दल युआन-शी-काई के निरंकुश शासन के विरुद्ध था। परिणामस्वरूप युआन-शी-काई से इस दल का संघर्ष आरंभ हो गया। 1921 ई० में कुओमीनतांग दल ने दक्षिणी चीन में कैंटन (Canton) सरकार की स्थापना की और डॉ० सन-यात-सेन को इस प्रकार का अध्यक्ष बनाया गया।
इसी समय इस दल के पुनर्गठन की फिर से आवश्यकता अनुभव की गई। अतः डॉ० सन-यात-सेन के प्रति निष्ठा आदि की शर्तों को हटा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस दल की सदस्य संख्या में काफी वृद्धि हुई।
2. कुओमीनतांग दल के सिद्धांत :
कुओमीनतांग दल के सिद्धांतों की व्याख्या अनेक अवसरों पर भाषणों. लेखों तथा दल के घोषणा-पत्र द्वारा की गई थी। 1924 ई० में द सम्मेलन बुलाया गया था। इससे पहले दल के सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया। दल के सिद्धांत डॉ० सन-यात-सेन के, जनता के तीन सिद्धांतों (Three Principles of the People) पर आधारित थे। इन तीन सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है
(1) राष्ट्रीयता :
डॉ० सन-यात-सेन के तीन सिद्धांतों में पहला सिद्धाँत राष्ट्रीयता का था। डॉ० सन-यात-सेन का यह विश्वास था कि जनता में राष्ट्रवाद का विकास होना बहुत आवश्यक है। वह प्रायः चीनी जनता की तुलना रेत के ढेर से करते थे, जिसके प्रत्येक कण में आपसी समानता तो विद्यमान है परंतु मज़बूती का पूर्ण अभाव है।
राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए वह साम्राज्यवाद का विरोध तथा राष्ट्रीय मोर्चों का निर्माण आवश्यक समझते थे। यह बात याद रखने योग्य है कि डॉ० सन-यात-सेन विदेश विरोधी नहीं थे। वह तो केवल विदेशी शक्तियों की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे।
(2) राजनीतिक लोकतंत्र :
डॉ० सन-यात-सेन का दूसरा सिद्धांत राजनीतिक लोकतंत्र था। वास्तव में 1911 ई० में चीन में अकस्मात् ही राज्य क्राँति हो गई थी और इस समय देश लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था। चीन के लोग भी लोकतंत्र को चलाने की योग्यता नहीं रखते थे, परंतु क्रांतिकारी नेता इस बात को समझ नहीं पाए थे। अतः जब वे इस बात को भली-भाँति समझ गए थे, उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए तीन बातों का सहारा लिया।
डॉ० सन-यात-सेन चाहते थे कि देश का शासन सेना के हाथ में रहे। दूसरे स्थान पर देश में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। तीसरी बात संवैधानिक सरकार की थी। देश का संविधान जनता द्वारा चुनी गई सभा के द्वारा तैयार किया जायेगा।
(3) जनता की जीविका :
डॉ० सन-यात-सेन का तीसरा सिद्धांत जनता की जीविका का था। डॉ० सन-यात-सेन चाहते थे कि चीन की जनता की भौतिक उन्नति हो। चीन की अधिकाँश जनता गाँवों में रहती थी और मुख्यतया कृषि पर निर्भर थी। चीन के ज़मींदारों और किसानों के बीच एक गहरी आर्थिक विषमता थी। वास्तव में देश की भौतिक उन्नति के लिए इस विषमता को दूर करना बहुत आवश्यक था।
अत: दल के कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि भूमि का समान वितरण करके किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बड़े उद्योगों का विकास करके उनकी पूँजी पर राज्य द्वारा नियंत्रण रखा जाए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक था ताकि विदेशी शक्तियों के द्वारा आर्थिक शोषण को रोका जा सके।
3. कुओमीनतांग में फूट:
1925 ई० में डॉ० सन-यात-सेन की मृत्यु के पश्चात् कुओमीनतांग के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न होने आरंभ हो गये। इस समय चियांग-काई-शेक (Chiang-Kai-Shek) ने सेना पर बहुत प्रभाव स्थापित कर लिया था। वह वाहम्पिया सैनिक अकादमी का डायरेक्टर (Director of Whampia Military Academy) था। सेना पर प्रभाव रखने के कारण उसका कैंटन पर काफी नियंत्रण था।
चियांग-काई-शेक ने मार्च, 1925 ई० में कैंटन में फ़ौजी कानून की घोषणा कर दी और उसने रूसी सलाहकारों को वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। वह स्वयं कैंटन सरकार का मुखिया बन गया। अनेक कारणों से साम्यवादियों तथा चियांग-काई-शेक के अनुयायियों में विरोध उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप कुओमीनतांग दल के प्रभाव में कुछ कमी आई।

प्रश्न 12.
1949 ई० की चीनी क्रांति के कारण तथा परिणाम बताएँ।
अथवा
1949 ई० की चीन की क्रांति के क्या कारण थे?
अथवा
1949 ई० की चीन की क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर
I. क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण
1949 ई० की क्राँति अकस्मात् ही नहीं आ गई थी। इस क्रांति के बीज 1911 ई० की क्रांति के समय ही बो दिए गए थे। 1911 ई० की क्रांति के पश्चात् चीन में ऐसा घटनाक्रम चला जो इसे 1949 ई० की ओर ले गया। इन घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. 1911 ई० की क्रांति :
1949 ई० की क्रांति के मूल कारण 1911 ई० की क्रांति में ही छुपे हुए थे। 1911 ई० की क्रांति के परिणामस्वरूप चीन में माँचू वंश का अंत हुआ तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। परंतु फिर भी राजसत्ता के लिए लगातार संघर्ष होता रहा। कई राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। इनमें से कुओमीनतांग नामक साम्यवादी दल सब से महत्त्वपूर्ण दल के रूप में उभरा। कई विदेशी शक्तियाँ जैसे रूस और जापान भी किसी-न-किसी रूप में चीन की राजनीति को प्रभावित करती रहीं। ये सभी घटनाएँ 1949 ई० की क्रांति की आधारशिला बनीं।
2. चार मई का आंदोलन :
1919 ई० में वर्साय (Versailles) पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में चीन को भारी निराशा हाथ लगी। शांति सम्मेलन के निर्णयों के परिणामस्वरूप चीनी लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्र चीन में जापान के प्रभाव को कम करने में असफल रहे थे। इस कारण चीन के लोग जापान के विरुद्ध हो गए। इस कारण 4 मई, 1919 ई० में 3000 से अधिक विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने पीकिंग (बीजिंग) के तियानमेन चौक (Tiananmen square) में एक भारी प्रदर्शन किया।
उन्होंने में शातंग (Shantang) पर दिए गए निर्णय की घोर आलोचना की। सरकार ने इस भीड पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग से काम लिया। इतिहास में यह घटना ‘चार मई दिवस’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना से चीनी लोगों में एक नई चेतना का संचार हुआ तथा 1949 ई० की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
3. वाशिंगटन सम्मेलन :
अमरीका के प्रयासों से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1921-22 ई० में वाशिंगटन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नौ देशों ने भाग लिया। इन नौ देशों ने वचन दिया कि चीन की एकता, अखंडता तथा स्वतंत्रता बनाए रखी जाएगी। यह भी कहा गया कि चीन में सभी देशों को समान रूप से व्यापारिक सुविधाएँ दी जाएँगी तथा 1 जनवरी, 1923 ई० तक सभी विदेशी डाक एजेंसियाँ समाप्त कर दी जाएँगी।
एक संधि के अनुसार जापान ने शातुंग प्रांत में अपनी सभी रियायतें त्याग दी तथा सभी विदेशी शक्तियों ने अपनी सेनाएँ चीन से निकाल लीं। इस सम्मेलन से चीन को एक नया जीवन मिला। इस सम्मेलन के पश्चात् विदेशी शक्तियों का चीन में प्रभाव कम हो गया तथा चीन को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। परंतु फिर भी चीन की सरकार जापान की साम्राज्यवादी गतिविधियों को कम न कर सकी। चीन सरकार की यही असमर्थता 1949 ई० की क्रांति का कारण सिद्ध हुई।
4. जापान द्वारा चीन पर आक्रमण :
1 जुलाई, 1937 ई० को जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 1945 ई० तक चला। इस आक्रमण के समय नानकिंग की सरकार तथा साम्यवादियों में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार उन्होंने मिल कर संयुक्त रूप से जापान का सामना करने का निर्णय लिया। यद्यपि इस युद्ध के दौरान चियांग-काई-शेक एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आया परंतु आठ वर्षों के इस लंबे युद्ध में चीन की पराजय से उसके समर्थक भी उसके शत्रु बन गए।
दूसरी ओर चियांग-काई-शेक भी साम्यवादियों को अपना शत्रु ही मानता रहा। फिर भी जापान के साथ युद्ध तथा द्वितीय महायुद्ध के दौरान साम्यवादियों का प्रभुत्व बना रहा। साम्यवादियों ने जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों पर मार्च, 1945 ई० में अपना अधिकार कर लिया।
5. चीन में गृहयुद्ध :
1945 ई० में जापान के पतन के पश्चात् जापान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों पर अधिकार जमाने के प्रश्न पर साम्यवादियों तथा कुओमीनतांग में आपसी होड़-सी लग गई। परिणामस्वरूप चीन में गृहयुद्ध छिड़ गया। तभी अमरीका के प्रयासों से माओ-त्सेतुंग तथा चियांग-काई-शेक आपसी बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रवादियों तथा साम्यवादियों में समझौता करवाने के लिए अपने विशेष दूत जॉर्ज मार्शल को भेजा। उसके प्रयासों से जनवरी 1946 ई० को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें राष्ट्रीय सरकार, साम्यवादियों तथा अमरीका के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। फ़रवरी, 1946 ई० में हुए एक समझौते के अनुसार राष्ट्रीय सरकार तथा साम्यवादियों ने अपनी सेनाओं में कमी कर दी। यह निर्णय भी किया गया कि दोनों सेनाएँ संयुक्त कर दी जाएँ और प्रत्येक प्रदेश में साम्यवादियों की सेना को अल्पमत में रखा जाए। परंतु दोनों दलों में सरकार के स्वरूप के प्रश्न पर दरार पड़ गई। राष्ट्रवादी शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में थे और साम्यवादी विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। इस प्रकार इस समस्या को न सुलझाया जा सका।
II. घटनाएँ
धीरे-धीरे साम्यवादी राष्ट्रवादियों पर हावी हो गए। 1946 ई० में राष्ट्रवादियों ने साम्यवादियों को उत्तर से खदेड़ दिया तथा वहाँ के मुख्य नगरों तथा रेलवे लाइनों पर अपना अधिकार जमा लिया। परंतु 1947 ई० में परिस्थितियाँ राष्ट्रवादियों के विरुद्ध हो गईं और साम्यवादियों ने उन्हें मंचूरिया के अधिकतर भागों से निकाल बाहर किया।
उन्होंने 1948 ई० में मुकदेन तथा 1949 ई० में तीनस्तीन और पीकिंग पर अपना अधिकार कर लिया। धीरे-धीरे उनका शंघाई, तथा हैंको आदि प्रदेशों पर भी अधिकार हो गया। उन्होंने 1 अक्तूबर, 1949 ई० में कैंटन पर अधिकार कर लिया जो कि राष्ट्रीय सरकार की राजधानी थी। इस प्रकार फारमोसा और कुछ द्वीपों को छोड़ कर सारे चीन पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया।
III. 1949 ई० की चीन की क्रांति के प्रभाव
1949 ई० की क्रांति को न केवल चीन बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस क्राँति ने जहाँ चीन के समाज को प्रभावित किया वहाँ विश्व भी इसके प्रभावों से अछूता न रहा। इस क्राँति के महत्त्वपूर्ण प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. शक्तिशाली केंद्रीय सरकार :
1949 ई० की क्राँति से चीन में एकता स्थापित हुई। केवल फारमोसा को छोड़ कर शेष सारा देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन लाया गया। राजनीतिक एकता के साथ-साथ सारे देश में एक प्रकार का ही शासन स्थापित किया गया। अब चीन अयोग्य तथा भ्रष्ट शासन से मुक्त हो चुका था । चीन वासी अब अपने पर गर्व कर सकते थे।
2. शाँति एवं सुरक्षा:
साम्यवादी सरकार की स्थापना से चीन में काफी समय से व्याप्त अराजकता एवं अव्यवस्था का अंत हुआ तथा पूर्ण स्थायी शाँति की स्थापना हुई। साम्यवादियों ने अपनी कुशल पुलिस व्यवस्था तथा गुप्तचर व्यवस्था से क्रांति का विरोध करने वालों तथा समाज विरोधी तत्त्वों का अंत कर दिया। इससे स्थायी शाँति की स्थापना हुई तथा लोग अपने-आप को सुरक्षित अनुभव करने लगे।
3. सामाजिक सुधार:
साम्यवादी सरकार ने अनेकों सामाजिक सुधार भी किए। उन्होंने समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों का अंत करके महान् कार्य किया। साम्यवादी सरकार ने चीन में अफ़ीम के प्रयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआबाजी आदि के विरुद्ध भी कानून बनाए गए। सरकार ने स्त्रियों के उत्थान की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। फलस्वरूप उन्हें सदियों पश्चात् चीनी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ।
4. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव :
1949 ई० की चीनी क्राँति से वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया। इस क्राँति से पूर्व छोटे किसानों की दशा बड़ी दयनीय थी तथा उनकी समस्याओं के प्रति सरकार उदासीन रहती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के पश्चात् भी उन्हें भर–पेट भोजन नसीब नहीं ता था। इसके विपरीत बडे-बडे जमींदार विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। 1949 ई० की क्रांति के पश्चात भमि का पुनर्विभाजन किया गया। बड़े ज़मींदारों से फालतू भूमि ले कर छोटे किसानों में बाँट दी गई। किसानों की दशा सुधारने के लिए सहकारी समितियाँ भी बनाई गईं।
प्रश्न 13.
माओ-त्सेतुंग के आरंभिक जीवन एवं सफलताओं के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
माओ-त्सेतुंग की गणना न केवल चीन अपितु विश्व के महान् व्यक्तित्वों में की जाती है। उसके आरंभिक जीवन एवं सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
I. आरंभिक जीवन
1. आरंभिक जीवन:
माओ-त्सेतुंग का जन्म 26 दिसंबर, 1893 ई० को चीन के हूनान (Hunan) प्रांत में स्थित एक छोटे से गाँव शाओ शां (Shao Shan) में हुआ था। उनके पिता का नाम माओ जेने-शुंग (Mao-Jane-Shung) था। वह एक गरीब किसान था। अतः उसे अपने जीवनयापन के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था। 15 वर्ष की आयु में माओ-त्सेतुंग ने अपना घर छोड़ दिया एवं एक स्कूल में प्रवेश ले लिया।
माओ के जीवन पर कांग यूवेई एवं लियांग किचाउ नामक प्रसिद्ध चीनी सुधारकों, वाशिंगटन, रूसो, नेपोलियन, पीटर महान्, अब्राहिम लिंकन आदि के जीवन का बहुत प्रभाव पड़ा। 1911 ई० की चीनी क्राँति के समय माओ-त्सेतुंग डॉक्टर सन-यात-सेन की क्रांतिकारी सेना में सम्मिलित हुआ था। उसने माँचू वंश का पतन होते हुए अपनी आँखों से देखा था।
माओ-त्सेतुंग 1917 ई० में हुई रूसी क्राँति से भी बहुत प्रभावित हुआ था। उसे पढाई से विशेष लगाव था इसलिए उसने पीकिंग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नौकरी कर ली। यहाँ उसने समाजवाद से संबंधित अनेक पुस्तकों को पढ़ा। 1921 ई० में चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इस समय माओ-त्सेतुंग इसका सदस्य बन गया था। शीघ्र ही वह इसके एक प्रमुख नेता बन गए।
2. लाँग मार्च 1934-35 ई०:
लाँग मार्च (लंबी यात्रा) चीन के इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1934 ई० में चियांग-काई-शेक जो कि साम्यवादियों को अपना कट्टर दुश्मन मानता था का विनाश करने के उद्देश्य से कियांग्सी (Kiangsi) का घेराव कर लिया। कियांग्सी उस समय साम्यवादियों का एक प्रमुख केंद्र था। इस घोर संकट के समय में माओ-त्सेतुंग ने बहुत साहस से कार्य लिया।
उसने अपने अधीन एक लाख लाल सेना (Red Army) एकत्रित की तथा वह चियांग-काई-शेक के घेराव को तोड़ते हुए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा 16 अक्तूबर, 1934 ई० को आरंभ की गई थी। उसने शांग्सी (Shanxi) तक का 6,000 मील का कठिन सफर तय किया। यह एक बहुत ज़ोखिम भरी यात्रा थी। रास्ते में उन्हें चियांग-काई-शेक की सेना का अनेक बार सामना करना पड़ा।
उन्हें भूखे-प्यासे अनेक वनों, नदियों एवं कठिन पर्वतों को पार करना पड़ा। इनके चलते करीब 80 हज़ार माओ के सैनिक रास्ते में मृत्यु का ग्रास बन गए। 370 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात् 20 अक्तूबर, 1935 ई० को माओ-त्सेतुंग अपने 20 हजार सैनिकों के साथ शांग्सी पहुँचने में सफल हुआ। निस्संदेह विश्व इतिहास में इस घटना की कोई उदाहरण नहीं मिलती। प्रसिद्ध इतिहासकार इमानूएल सी० वाई० सू के अनुसार, “यह साम्यवादी पार्टी के इतिहास की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी तथा माओ की शक्ति को शिखर तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध हुई।”
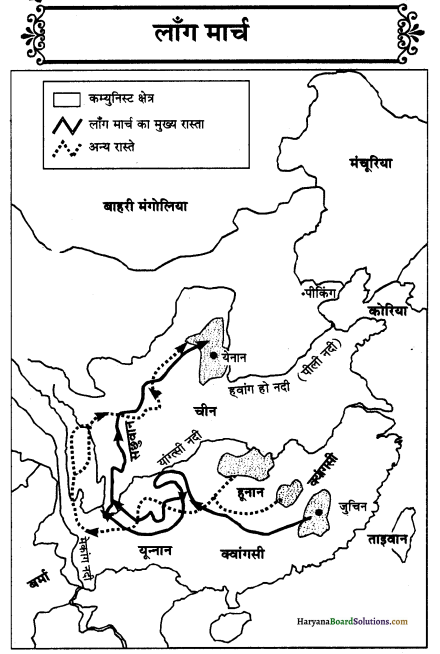
II. माओ-त्सेतुंग की सफलताएँ
माओ-त्सेतुंग एवं साम्यवादी दल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप चीन में अंतत: 1 अक्तूबर, 1949 ई० को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (People’s Republic of China) की स्थापना हुई। निस्संदेह इससे चीनी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। चीनी लोगों को एक शताब्दी के पश्चात् विदेशी शक्तियों के शोषण से मुक्ति मिली। इस अवसर पर माओ-त्सेतुंग को चीनी गणराज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसने अपने शासनकाल (1949-76 ई०) के दौरान अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. राजनीतिक एकता की स्थापना:
माओ-त्सेतुंग ने सत्ता संभालने के पश्चात् अपना सर्वप्रथम विशेष ध्यान चीन में राजनीतिक एकता स्थापित करने की ओर दिया। चीन जैसे विशाल देश को एकता के सूत्र में बाँधना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए माओ-त्सेतुंग ने बल एवं कूटनीति दोनों का प्रयोग किया। इस उद्देश्य में वह काफ़ी सीमा तक सफल रहा।
2.1954ई० का संविधान:
चीन में 20 सितंबर, 1954 ई० को एक नया संविधान लागू किया गया। इसमें राष्ट्रीय जन कांग्रेस (National People’s Congress) को राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था घोषित किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 1200 रखी गई। इनका चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता था। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष बुलाया जाता था। अध्यक्ष को देश का राष्ट्राध्यक्ष (Head of the State) घोषित किया गया। इस पद पर माओ-त्सेतुंग नियुक्त हुए।
उन्हें विशाल अधिकार दिए गए। संविधान द्वारा साम्यवादी दल को सर्वोच्च स्थान दिया गया। राज्य के सभी प्रमुख पद साम्यवादी दल के नेताओं को दिए गए। चाऊ एनलाई (Zhou Enlai) को देश का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों एवं न्याय व्यवस्था पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है।
3. आर्थिक प्रगति:
माओ-त्सेतुंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण पग उठाए। उसने विदेशी पूँजी एवं उनके द्वारा स्थापित कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। दसरा सरकार ने छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया। उसने श्रमिकों की दशा सुधारने के उद्देश्य से उनकी मजदूरी बढ़ा दी।
उसने मुद्रा संबंधी कार्यों तथा ऋण के संचालन के लिए 1950 ई० बैंक ऑफ़ चाइना (People’s Bank of China) की स्थापना की उसने चीन में आर्थिक विकास के उद्देश्य से चीन की सरकार ने रूस की सरकार से सहायता प्राप्त की। उसने चीन में विशाल उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से 1953 ई० में प्रथम पँचवर्षीय योजना आरंभ की।
4. लंबी छलाँग वाला आंदोलन :
1958 ई० में चीन में लंबी छलाँग वाला आंदोलन चलाया गया। इसका उद्देश्य चीन में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीन में कम्यून्स (Communes) की स्थापना की गई। 1958 ई० के अंत तक चीन में ऐसे 26,000 कम्यून्स की स्थापना की जा चुकी थी। प्रत्येक कम्यून में लगभग 5,000 परिवार होते थे। इनके अपने खेत एवं कारखाने आदि होते थे।
प्रत्येक कम्यून उत्पादन, वितरण एवं खपत आदि पर नज़र रखता था। यद्यपि सरकार द्वारा लगातार इस आंदोलन की सफलता की घोषणा की गई किंतु वास्तविकता यह थी कि यह विफल रहा। लीऊ शाओछी (Liu Shaochi) एवं तंग शीयाओफींग (Deng Xiaoping) नामक नेताओं ने कम्यून प्रथा को बदलने का प्रयास किया क्योंकि ये कुशलता से काम नहीं कर रही थीं।
अत: 1959 ई० में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार जे० डब्ल्यूक हाल का यह कहना ठीक है कि, “लंबी छलाँग वाला आंदोलन विफल रहा तथा इसने अपने पीछे आर्थिक महामंदी तथा भारी मानव दुःखों को छोड़ा।”
5. शिक्षा का प्रसार :
माओ-त्सेतुंग शिक्षा के महत्त्व को अच्छी प्रकार से जानता था। अतः उसने शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इस उद्देश्य से उसने संपूर्ण चीन में अनेक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। किसानों एवं मजदूरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया।
चीन में तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया ताकि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् बेरोज़गार न रहें। इसलिए पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन किए गए।
6. स्त्रियों की स्थिति में सुधार:
1949 ई० से पूर्व चीन में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया था। माओ-त्सेतुंग के शासनकाल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक पग उठाए गए। प्रथम, उन्हें भूमि की स्वामिनी बना दिया गया। अतः उन्हें अपनी जीविका के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था।
दूसरा, चीन के संविधान के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सभी प्रकार के अधिकार दिए गए। तीसरा, 1950 ई० के विवाह कानून के अनुसार एक विवाह की प्रथा प्रचलित की गई। तलाक का अधिकार दोनों पति एवं पत्नी को समान रूप से दिया गया। चीन में वेश्यावृत्ति का उन्मूलन कर दिया गया। राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर स्त्रियों को नियुक्त किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप चीन की स्त्रियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
7. महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति :
माओ-त्सेतुंग चीन में एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में विफल रहा। अतः सरकार के विरोधियों ने उसकी आलोचना करनी आरंभ कर दी। माओ इसे सहन करने को तैयार नहीं था। अतः उसने अपने विरोधियों का सफाया करने के उद्देश्य से 1966 ई० में महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्राँति को आरंभ किया।
इसके अधीन रेड गाईस (लाल रक्षक) का गठन किया गया। इसमें छात्रों एवं सैनिकों को भर्ती किया गया। उन्होंने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों एवं पुरानी आदतों के खिलाफ एक ज़ोरदार आंदोलन आरंभ किया। सभी माओ विरोधियों का निर्ममतापूर्वक दमन किया गया। उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया। शीघ्र ही सांस्कृतिक क्राँति ने एक उग्र रूप धारण कर लिया। इससे संपूर्ण चीन में अराजकता फैल गई। इसके बावजूद इसे 1976 ई० में माओ-त्सेतुंग की मृत्यु तक जारी रखा गया।

प्रश्न 14.
जापान एवं चीन में आधुनिकता के अपनाए गए मार्गों का संक्षिप्त वर्णन करें। क्या इनमें कोई अंतर है?
उत्तर:
जापान एवं चीन ने आधुनिकता के अलग-अलग मार्ग अपनाए। इन मार्गों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है
1. जापान द्वारा अपनाया गया मार्ग:
जापान ने 19वीं शताब्दी तक चीन की तरह पश्चिमी देशों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। उसने विदेशियों के साथ कोई संपर्क नहीं रखा था। 1853 ई० में अमरीका के कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के जापान आगमन से जापान के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस समय जापान ने अमरीका के साथ राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करने का निर्णय किया। अतः 1854 ई० में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी एवं जापान की सरकार के मध्य कानागावा की संधि हो गई।
इस संधि के अनुसार जापान ने शीमोदा (Shimoda) एवं हाकोदाते (Hakodate) नामक दो बंदरगाहों को अमरीका के जहाजों के लिए खोल दिया। शीमोदा में अमरीका के वाणिज्य दूत को रहने की अनुमति दे दी गई। जापान ने अमरीका के साथ सबसे अच्छे राष्ट्र जैसा व्यवहार करने का वचन दिया।
अमरीका के पदचिन्हों पर चलते हुए हालैंड, ब्रिटेन, रूस एवं फ्राँस ने भी जापान के साथ संधियाँ कर ली तथा वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए जो जापान ने अमरीका को दिए थे। जापान ने इन पश्चिमी देशों के साथ ये संधियाँ अपनी इच्छा एवं बराबरी के आधार पर की थीं। इन संधियों द्वारा जापान पश्चिमी देशों का ज्ञान प्राप्त कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता था।
जापान में आधुनिकीकरण का नेतृत्व कुलीन वर्ग ने किया। इनके अधीन जापान ने एक उग्र राष्ट्रवाद (aggressive nationalism) को जन्म दिया। उन्होंने शोषणकारी सत्ता (repressive regime) को जारी रखा। उन्होंने लोकतंत्र की माँग को कुचल दिया तथा विरोध के स्वर को उठने नहीं दिया। जापान ने सैन्यवादियों के प्रभाव के चलते एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की। इस कारण उसे अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा। इसके चलते उसके विकास में बाधा आई।
जापान के आधुनिकीकरण में उसकी सांस्कृतिक परंपराओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इनका उपयोग नए रचनात्मक ढंग से किया गया। मेज़ी काल में विद्यार्थियों को यूरोपीय एवं अमरीकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों को पढ़ाया जाने लगा। किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जापानी निष्ठावान नागरिक बनें। अत: जापान में नैतिक शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया।
इसमें सम्राट् के प्रति वफ़ादारी पर विशेष बल दिया जाता था। जापान के लोगों ने रोज़मर्रा की जिंदगी में भी केवल पश्चिमी समाजों की अंधाधुंध नकल नहीं की अपितु उन्होंने देशी एवं विदेशी को मिलाया। इसका उदाहरण जापानी लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी में आए बदलावों से लगाया जा सकता है।
2. चीन द्वारा अपनाया गया मार्ग:
चीन का आधुनिकीकरण का सफर जापान से काफी भिन्न था। चीन ने पश्चिमी देशों से अपनी दूरी बनाए रखी। परिणामस्वरूप पश्चिमी देशों को जब अफ़ीम के युद्धों के पश्चात् चीन की वास्तविक कमजोरी का ज्ञान हुआ तो अनेक देश लूट की होड़ में सम्मिलित हो गए। इसके चलते चीनी लोगों को अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा। प्राकृतिक त्रासदियों ने लोगों के दुःखों को और बढ़ा दिया।
1949 ई० में चीन में साम्यवादी दल के सत्ता में आने से वहाँ एक नए युग का श्रीगणेश हुआ। इसने चीन में राजनीतिक एकता स्थापित की। चीनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विशेष पग उठाए गए। साम्यवादी दल एवं उसके समर्थकों ने परंपरा का अंत करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनका विश्वास था कि परंपरा के कारण ही जनसाधारण गरीबी में जकड़ा हुआ है एवं देश अविकसित है। इस कारण ही स्त्रियों की दशा दयनीय है। अतः साम्यवादी दल ने शिक्षा में अनिवार्य बदलाव किए ताकि लोगों के दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन आए।
उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें अनेक अधिकार दिए। चीन में वेश्यावृति का उन्मूलन कर दिया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप चीन में आज स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आज चीनी समाज में पुनः असमानताएँ उभर रही हैं तथा परंपराएँ पुनर्जीवित होने लगी हैं। अतः चीन की आज सबसे बड़ी चुनौती इन समस्याओं से निपटने की है।
क्रम संख्या
Table
संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न
प्रश्न 1.
जापान की भौगोलिक विशेषताएँ लिखें।
उत्तर:
जापान प्रशांत महासागर की गोद में बसा हुआ पूर्वी एशिया का एक महान् देश है। इसे विश्व का एक अत्यंत सुंदर एवं रमणीय देश माना जाता है। इसका कारण यह है यहाँ की जलवायु बहुत स्वच्छ है। यहाँ वर्षा काफी होती है। यहाँ जंगलों, नदियों, झीलों एवं पर्वतों की बहुतायत है। जापान 3000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से अधिकांश द्वीप छोटे हैं।
जापान के चार द्वीप होश, क्यूश, शिकोकू तथा होकाइदो प्रमुख हैं। इन द्वीपों में होंशू सबसे बड़ा है तथा जापान का केंद्र है। यहाँ जापान की राजधानी एदो (आधुनिक तोक्यो) सहित कुछ अन्य प्रसिद्ध नगर स्थित हैं। क्यूशू द्वीप चीन के निकट स्थित होने के कारण यह सर्वप्रथम यूरोप के संपर्क में आया।
प्रश्न 2.
शोगुन कौन थे ? उनकी सफलताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
शोगुन जापान के सम्राट् के प्रधान सेनापति थे। 1603 ई० में तोकुगावा वंश के लोगों ने शोगुन पद पर अधिकार कर लिया था। वह इस पद पर 1867 ई० तक कायम रहे। इस समय के दौरान उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की। उन्होंने अपने विरोधियों को पराजित कर जापान में कानून व्यवस्था को लागू किया। उन्हेंने दैम्यों पर कड़ा नियंत्रण रखा तथा उन्हें शक्तिशाली न होने दिया।
उन्होंने प्रमुख शहरों एवं खादानों पर भी नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने योद्धा वर्ग जिसे समुराई कहा जाता था को विशेष सुविधाएँ प्रदान की। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों से हथियार वापस ले लिये। उन्होंने भूमि की उत्पादन शक्ति के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित किया।
प्रश्न 3.
कॉमोडोर मैथ्यू पेरी कौन था ? उसके जापान आगमन का क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर:
1852 ई० में अमरीका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापान की सरकार के साथ एक समझौता करने के लिए भेजा। इसका उद्देश्य अमरीका एवं जापान के मध्य राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। पेरी जापान की सरकार के साथ 31 मार्च, 1854 ई० को कानागावा की संधि करने में सफल हो गया। इस संधि के अनुसार जापान की दो बंदरगाहों शीमोदा एवं हाकोदाटे को अमरीका के लिए खोल दिया गया।
शीमोदा में ” अमरीका के वाणिज्य दूत को रहने की अनुमति दी गई। जापान ने अमरीका के साथ बहुत अच्छे राष्ट्र जैसा व्यवहार करने का वचन दिया। विदेशियों के प्रवेश से जापान में स्थिति ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया। शोगुन इस स्थिति को अपने नियंत्रण में लाने में विफल रहे। अत: उन्हें अपने पद को त्यागना पड़ा।
प्रश्न 4.
मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएँ क्या थीं, जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया ?
उत्तर:
(1) 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में शहरों के तीव्र विकास से व्यापार एवं वाणिज्य को बहत बल मिला। इससे व्यापारी वर्ग बहुत धनी हुआ। इस वर्ग ने जापानी कला एवं साहित्य को एक नई दिशा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
(2) तोकुगावा काल में जापान के लोगों में शिक्षा का काफी प्रचलन था। अनेक लोग केवल लेखन द्वारा ही अपनी जीविका चलाते थे। पुस्तकों का प्रकाशन बड़े स्तर पर किया जाता था। 18वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों की अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया गया। इससे जापान के लोगों को पश्चिम के ज्ञान के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
(3) तोकुगावा काल में जापान एक धनी देश था। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान चीन से रेशम तथा भारत से वस्त्र आदि विलासी वस्तुओं का आयात करता था। इसके बदले वह सोना एवं चाँदी देता था। इसका जापानी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण तोकुगावा को इन कीमती वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। उन्होंने रेशम के आयात को कम करने के उद्देश्य से 16वीं शताब्दी में निशिजन में रेशम उद्योग की स्थापना की।
प्रश्न 5.
मेजी शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी ?
उत्तर:
(1) मेजी सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता जापान में सामंती प्रथा का अंत करना था। मेजी, सरकार ने 1871 ई० में जापान में सामंती प्रथा के अंत की घोषणा की। इस प्रथा के अंत से जापान आधुनिकीकरण की दिशा की ओर अग्रसर हुआ।
(2) मेजी पुनर्स्थापना के पश्चात् जापान में उल्लेखनीय शिक्षा सुधार किए गए। इससे पूर्व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल समाज के उच्च वर्ग को ही प्राप्त था। जापान में 1871 ई० में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से प्रगति हुई।
(3) मेजी काल में सेना को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। 1872 ई. में 20 वर्ष से अधिक नौजवानों के लिए सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। नौसेना को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया।
(4) जापान में उद्योगों के विस्तार की ओर सरकार ने अपना विशेष ध्यान दिया। इस उद्देश्य से 1870 ई० में जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना जापानी उद्योगों के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुआ।
(5) मेज़ी काल में कृषि क्षेत्र में भी प्रशंसनीय सुधार किए गए। सामंती प्रथा का अंत हो जाने से किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई।
(6) मेज़ी काल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 1889 ई० में एक नए संविधान को लागू करना था। इस संविधान के अनुसार सम्राट् को सर्वोच्च सत्ता सौंपी गई। उसे कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे।
प्रश्न 6.
मेज़ी शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय सुधार बताएँ।
उत्तर:
मेजी पुनर्स्थापना के पश्चात् जापान में उल्लेखनीय शिक्षा सुधार किए गए। जापान में 1871 ई० में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से प्रगति हुई। संपूर्ण जापान में अनेक स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। 6 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 1877 ई० में जापान में तोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम की प्रसिद्ध पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया। 1901 ई० में जापानी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में एक मील पत्थर सिद्ध हुआ।
प्रश्न 7.
मेज़ी काल के मुख्य आर्थिक सुधारों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
उत्तर:
(1) औद्योगिक विकास-जापान में उद्योगों के विस्तार की ओर सरकार ने अपना विशेष ध्यान दिया। इस उद्देश्य से 1870 ई० में जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना जापानी उद्योगों के विकास के लिए एक मील पत्थर सिद्ध हुई। सरकार ने भारी उद्योगों के विकास के लिए पूँजीपतियों को प्रोत्साहित किया। अतः जापान में शीघ्र ही अनेक नए कारखाने स्थापित हुए। इनमें लोहा-इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, जहाज़ उद्योग एवं शस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे।
(2) कृषि सुधार-मेज़ी काल में कृषि क्षेत्र में भी प्रशंसनीय सुधार किए गए। सामंती प्रथा का अंत हो जाने से किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो गई। 1872 ई० में सरकार के एक आदेश द्वारा किसानों को उस भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। किसानों से बेगार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसानों को कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई। उन्हें उत्तम किस्म के बीज दिए गए। पशुओं की उत्तम नस्ल का प्रबंध किया गया। किसानों से अब अनाज की अपेक्षा नकद भू-राजस्व लिया जाने लगा। उन्हें कृषि के पुराने ढंगों की अपेक्षा आधुनिक ढंग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
(3) कुछ अन्य सुधार-जापान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेज़ी काल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। सर्वप्रथम यातायात के साधनों का विकास किया गया। 1870-72 ई० में जापान में तोक्यो एवं योकोहामा के मध्य प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। जहाज़ निर्माण के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति की गई। द्वितीय, मुद्रा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। तीसरा, 1872 ई० में जापान में बैंकिंग प्रणाली को आरंभ किया गया। 1882 ई० में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई।
प्रश्न 8.
मेज़ी संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या थी ?
उत्तर:
मेज़ी काल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 1889 ई० में एक नए संविधान को लागू करना था। इस संविधान के अनुसार सम्राट को सर्वोच्च सत्ता सौंपी गई। उसे कई प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। संपूर्ण सेना उसके अधीन थी। उसे किसी भी देश से युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार दिया गया था। वह डायट (संसद्) के अधिवेशन को बुला सकता था तथा उसे भंग भी कर सकता था। वह सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता था तथा वे अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होते थे।
केवल सम्राट् ही मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता था। डायट का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष तीन माह के लिए बुलाया जाता था। इसमें सदस्यों को बहस करने का अधिकार प्राप्त था। सम्राट् डायट की अनुमति के बिना लोगों पर नए कर नहीं लगा सकता था। नए संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे। इसके अनुसार उन्हें भाषण देने, लिखने, एकत्र होने, संगठन बनाने एवं किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर माना जाता था।
प्रश्न 9.
जापान के विकास के साथ-साथ वहाँ की रोज़मर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए ? चर्चा कीजिए।
उत्तर:
मेज़ी शासनकाल में जापानियों की रोज़मर्रा की जिंदगी में अनेक महत्त्वपूर्ण बदलाव आए। मेज़ी काल से पूर्व जापान में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। मेज़ी काल में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ने लगा। इसमें पति, पत्नी एवं उनके बच्चे रहते थे। अतः वे नए घरों जिसे जापानी में होमु कहते थे में रहने लगे।
वे घरेलू उत्पादों के लिए बिजली से चलने वाले कुकर, माँस एवं मछली भूनने के लिए अमरीकी भूनक तथा ब्रेड सेंकने के लिए टोस्टर का प्रयोग करने लगे। जापानियों में अब पश्चिमी वेशभूषा का प्रचलन बढ़ गया। वे अब सूट एवं हैट डालने लगे। औरतों के लिबास में भी परिवर्तन आ गया। वे अब सौंदर्य वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देने लगीं। परस्पर अभिवादन के लिए हाथ मिलाने का प्रचलन लोकप्रिय हो गया। मनोरंजन के नए साधनों का विकास हुआ। लोगों की सुविधा के लिए विशाल डिपार्टमैंट स्टोर बनने लगे। 1899 ई० में जापान में सिनेमा का प्रचलन आरंभ हुआ।

प्रश्न 10.
1894-95 ई० के चीन-जापान के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे ?
उत्तर:
(1) रूस के कोरिया में बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जापान को चिंता हुई। जापान ने स्वयं वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास तीव्र कर दिए।
(2) कोरिया की आंतरिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह एक निर्बल देश था। उस समय कोरिया में अशांति फैली हुई थी तथा अव्यवस्था व्याप्त थी। जापान को हर समय भय लगा रहता था कि कोई अन्य देश कोरिया पर अपना अधिकार न कर ले। चीन भी अपने वंशानुगत अधिकार के कारण किसी अन्य देश के कोरिया में हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकता था।
(3) कोरिया में जापान के बढ़ रहे प्रभाव को देखकर चीन बहुत चिंतित हो गया। जापान के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से उसने विदेशी शक्तियों को कोरिया में व्यापार करने के प्रयासों में अपना समर्थन दिया।
(4) चीन-जापान यद्ध के कारणों में एक कारण कोरिया में जापान के आर्थिक हित भी थे। अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वह कोरिया की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहा था।
(5) कोरिया में ‘तोंगहाक’ संप्रदाय द्वारा किया गया विद्रोह चीन-जापान युद्ध का तत्कालीन कारण बना। इस संप्रदाय के लोग विदेशियों को पसंद नहीं करते थे। कोरिया सरकार इस संप्रदाय के विरुद्ध थी तथा उसने एक, अध्यादेश द्वारा उसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जापानी सेनाओं ने कोरिया के राजा को बंदी बना लिया। इस प्रकार 1 अगस्त, 1894 ई० को यह युद्ध आरंभ हुआ।
प्रश्न 11.
शिमोनोसेकी की संधि क्यों व कब हुई ? इसके क्या परिणाम निकले ?
उत्तर:
शिमोनोसेकी की संधि 17 अप्रैल, 1895 ई० को चीन एवं जापान के मध्य हुई। इस संधि की मुख्य धाराएँ अग्रलिखित अनुसार थीं
- चीन ने कोरिया को एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी।
- चीन ने पोर्ट आर्थर, फारमोसा, पेस्काडोरस तथा लियाओतुंग जापान को दे दिए।
- चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को 2 करोड़ तायल देगा।
- चीन जापान को सर्वाधिक प्रिय देश स्वीकार करेगा।
- चीन जापान के व्यापार के लिए अपनी चार बंदरगाहें शांसी, सो चाऊ, चुंग-किंग तथा हंग चाओ खोलेगा।
- जब तक चीन युद्ध की क्षतिपूर्ति की राशि जापान को नहीं चुकाएगा उसकी वी-हाई-वी नामक बंदरगाह जापान के पास रहेगी।
शिमोनोसेकी की संधि के कागजों पर अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि उसके 6 दिन पश्चात् ही फ्राँस, रूस तथा जर्मनी ने जापान को कहा कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीप चीन को लौटा दे। विवश होकर जापान ने शिमोनोसेकी की संधि में संशोधन करना मान लिया। उसने लियाओतुंग प्रायद्वीप चीन को वापस कर दिया।
प्रश्न 12.
1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध के कोई चार प्रमुख प्रभाव बताएँ।
उत्तर:
(1) जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि-जापान एशिया का एक छोटा सा देश था तथा चीन सबसे बड़ा देश था। फिर भी जापान ने चीन को पराजित कर दिया। इस युद्ध में विजय से जापान की प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गए। सभी यूरोपीय शक्तियों को विश्वास था कि जापान पराजित होगा। परंतु उसकी विजय ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। परिणामस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई।
(2) चीन की लूट आरंभ-जापान के हाथों पराजित होने से चीन की दुर्बलता सारे विश्व के आगे प्रदर्शित हो गई। इस कारण यूरोपीय शक्तियों की मनोवृत्ति में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। पहले पश्चिमी देशों ने चीन से कई प्रकार की रियायतें प्राप्त की हुई थीं। परंतु अब वे उसके साम्राज्य का विभाजन चाहने लगीं। अतः ये सभी देश चीन की लूट में जापान के भागीदार बनने के लिए तैयार हो गए।
(3) आंग्ल-जापानी समझौते की आधारशिला-चीन-जापान युद्ध के परिणामस्वरूप आंग्ल-जापानी समझौत (1902 ई०) की नींव रखी गई। जब जापान इस युद्ध में विजयी हो रहा था तो इंग्लैंड के समाचार-पत्रों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उनके अनुसार इंग्लैंड और जापान के हित सामान्य थे। अतः वे जापान को भविष्य का उपयोगी मित्र मानने लरो । जापान भी इंग्लैंड से मित्रता करना चाहता था। इस प्रकार ये दोनों देश एक-दूसरे के निकट आए तथा 1902 ई० में एक समझौता किया।
(4) जापान-रूस शत्रता-शिमोनोसेकी की संधि के पश्चात रूस जापान के विरुद्ध हो गया। उसने फ्राँस तथा जर्मनी के साथ मिल कर जापान पर दबाव डाला कि वह लियाओतुंग प्रायद्वीय चीन को वापस कर दे। इससे जापान रूस से नाराज़ हो गया। इसके अतिरिक्त चीन-जापान युद्ध के पश्चात् जापान भी रूस के समान दूर-पूर्व में एक शक्ति के रूप में उभरा। दोनों देश महत्त्वाकांक्षी थे और यही महत्त्वाकांक्षा उन्हें 1904-05 के युद्ध की ओर ले गई।
प्रश्न 13.
रूस-जापान युद्ध 1904-1905 के क्या कारण थे ?
उत्तर:
(1) 1894-95 ई० में हुए चीन-जापान युद्ध में जापान ने चीन को पराजित करके एक शानदार विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के पश्चात् हुई शिमोनोसेकी की संधि के अनुसार चीन ने अपने कुछ क्षेत्र जापान को दिए थे। इन प्रदेशों में एक लियाओतुंग प्रदेश भी था। उस संधि के कुछ दिनों पश्चात् ही रूस ने जापान पर दबाव डाला कि वह लियाओतुंग का प्रदेश चीन को वापस कर दे।
(2) चीन में हुए रियायतों के लिए संघर्ष में रूस सब से महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल रहा था। उसने 1898 ई० में लियाओतुंग का प्रदेश भी चीन से पट्टे पर ले लिया था। रूस की इस कार्यवाही से जापान भड़क उठा था।
(3) मंचूरिया भी रूस-जापान युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना। मंचूरिया चीन के उत्तरी भाग में स्थित था तथा ये दोनों देश उसमें रुचि रखते थे। उसने मंचूरिया में रेलवे लाइनें बिछाईं। अत: जापान ने रूस को एक सबक सिखाने का निर्णय किया।
(4) 1902 ई० में जापान तथा इंग्लैंड ने एक गठबंधन किया। इसके अधीन दोनों ने एक-दूसरे को वचन दिया कि चीन और कोरिया में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक-दूसरे को सहयोग देंगे। इंग्लैंड का इस आश्वासन से जापान को प्रोत्साहन मिला और उसने रूस के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी।
(5) जापान रूस की विस्तारवादी नीति से बड़ा चिंतित था। वह कोरिया तथा मंचूरिया के प्रश्न पर रूस से कोई समझौता करना चाहता था। अंततः दोनों के मध्य 10 फरवरी, 1904 ई० को युद्ध आरंभ हो गया।
प्रश्न 14.
जापान में सैन्यवाद के उत्थान के क्या कारण थे ?
उत्तर:
(1) जापान में सैन्यवादियों को एक के बाद एक सफलता प्राप्त होती गई जिसके कारण वे महत्त्वाकांक्षी हो गए। वे पूरे महाद्वीप पर नियंत्रण करना चाहते थे।
(2) बहुत-से पुराने नेता सैन्यवादियों की गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे। वास्तव में वे सैन्यवादियों पर अंकुश रखते थे। परंतु ज्यों-ज्यों समय गुज़रता गया वे बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण सैन्यवादियों पर जो उनका अंकुश था वह समाप्त हो गया और वे अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो गये।
(3) जापान में नवयुवक अधिकारियों की एक नई श्रेणी का उदय हुआ। ये नवयुवक अधिकारी अपनी शानदार विजयों द्वारा समाज में अपना स्थान बनाना चाहते थे। वे जापानी सैन्यवाद में विश्वास करते थे और शक्ति का प्रयोग करना अपना अधिकार समझते थे।
(4) सैन्यवादियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जापान में बहुत-सी गुप्त समितियों की स्थापना की गई थी। इनके उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार है-
(5) ये समितियाँ चाहती थीं कि जापान सारी दुनिया पर शासन करे। यदि ऐसा न हो सका तो जापान को समस्त देशों को विजय करना चाहिए।
(6) ये समितियाँ उदारवाद तथा प्रजातंत्र के विरुद्ध थीं। अतः इनका एक अन्य उद्देश्य पाश्चात्य देशों के सिद्धांतों का विरोध करना था।
(7) इन समितियों के सदस्य नाजीवाद तथा फासिस्टवाद में विश्वास रखते थे। वे फासिस्ट लोगों तथा नाजियों की भाँति राज्य को व्यक्ति से ऊपर मानते थे।
प्रश्न 15.
द्वितीय विश्व युद्ध का जापान पर क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर:
दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान की पराजय हुई। इस पराजय के परिणामस्वरूप जापान पूर्व का अधिपति बनने के प्रयत्न में असफल रहा। युद्ध में पराजित होकर जापान का प्रदेश संकुचित होकर 1894-95 ई० की स्थिति में आ गया अर्थात् जितना कि यह चीन और जापान के युद्ध के पश्चात् बना था। जापान के पास केवल चार मुख्य द्वीप तथा कुछ छोटे द्वीप रह गए।
कोरिया को अस्थायी तौर पर रूस तथा अमरीका ने बाँट लिया। फार्मोसा चीन को लौटा दिया गया। मित्र देशों की सेना ने जनरल मेकार्थर के अधीन जापान पर अधिकार कर लिया। जापान में शासन प्रबंध के लिए एक नई सरकार स्थापित की गई, परंतु वास्तविक सत्ता मेकार्थर के हाथ में थी, क्योंकि वह मित्र शक्तियों की ओर से सर्वोच्च कमांडर था। जापानी सरकार भी साथ चलती रही तथा इसी सरकार की सहायता से जनरल मेकार्थर अपनी नीति चलाता था। वास्तव में जापान अपनी आंतरिक तथा बाह्य स्वतंत्रता का बहुत बड़ा भाग खो चुका था।
प्रश्न 16.
1960 ई० के पश्चात् जापान की प्रगति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
1960 ई० के दशक से जापान प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहा। 1964 ई० में जापान की राजधानी तोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के आयोजन में जापान ने 3 करोड़ डालर खर्च किए। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस समय तक जापान की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो चुकी थी।
इसी वर्ष जापान में शिंकासेन नामक 200 मील प्रति घंटे की रफ़तार वाली रेलगाड़ी आरंभ हुई। इसे बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इससे जापान की नयी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी प्राप्त होती है। 1960 ई० के दशक में जापान में नागरिक समाज आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन के आरंभ होने का कारण यह था कि औद्योगीकरण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे थे।
1960 ई० के दशक में मिनामाता में पारे के जहर के फैलने तथा 1970 ई० के दशक में हवा के प्रदूषण से नयी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। इन समस्याओं से निपटने के लिए जापान की सरकार ने 1990 ई० के दशक में कछ कठोर पग उठाए।

प्रश्न 17.
प्रथम अफ़ीम युद्ध पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
प्रथम अफ़ीम युद्ध चीन तथा ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध 1839 ई० से लेकर 1842 ई० तक चला। ब्रिटेन यूरोप की एक प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति था तथा वह चीन में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1800 ई० में उसने चीन में भारत से लाकर अफ़ीम बेचनी आरंभ कर दी थी। 1839 ई० तक उसका अफ़ीम का व्यापार बहुत बढ़ गया था।
अफ़ीम के इस व्यापार के कारण चीनियों का नैतिक पतन होने लगा तथा उसकी सैनिक शक्ति शिथिल पड़ने लगी। इससे चिंतित होकर चीन के शासकों ने अफ़ीम के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किए। परंतु ब्रिटेन ने अपना व्यापार जारी रखा। 1839 ई० में चीनियों ने ब्रिटेन के अफ़ीम से भरे जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। परिणामस्वरूप चीन तथा ब्रिटेन में प्रथम अफ़ीम युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 29 अगस्त, 1842 ई० को हुई नानकिंग की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार
- चीन को युद्ध हर्जाने के रूप में 21 मिलियन डालर की राशि ब्रिटेन को देनी पड़ी।
- हांगकांग का द्वीप सदा के लिए ब्रिटेन को मिल गया।
- कैंटन के अतिरिक्त फूचाओ, अमोय, निंगपो तथा शंघाई नामक बंदरगाहें भी ब्रिटेन के लिए खोल दी गईं।
प्रश्न 18.
नानकिंग की संधि कब हुई ? इसकी प्रमुख धाराएँ क्या थी ?
उत्तर:
अंग्रेजों तथा चीनियों के बीच नानकिंग की संधि 29 अगस्त, 1842 ई० को हुई। इस संधि की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थीं
- हांगकांग का द्वीप सदा के लिए ब्रिटेन को सौंप दिया गया।
- ब्रिटिश लोगों को पाँच बंदरगाहों-कैंटन, अमोय, फूचाओ, निंगपो और शंघाई में बसने तथा व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया।
- क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने दो करोड़ दस लाख डालर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया।
- को-होंग को भंग कर दिया गया। परिणामस्वरूप अब ब्रिटिश व्यापारी किसी भी चीनी व्यापारी के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था।
- आयात और निर्यात पर एक समान तथा उदार दर स्वीकार कर ली गई।
- चीनियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अंग्रेज़ों के मुकद्दमे अंग्रेज़ी कानून के अनुसार तथा उन्हीं की अदालतों में चलेंगे।
- यह भी शर्त रखी गई कि चीन अन्य देशों के लोगों को जो भी सुविधाएँ देगा वे अंग्रेजों को भी प्राप्त होंगी।
प्रश्न 19.
द्वितीय अफ़ीम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था ?
उत्तर:
1856 ई० में घटने वाली लोर्चा ऐरो घटना द्वितीय अफ़ीम युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। 8 अक्तूबर, 1856 ई० में चीनी अधिकारियों ने लोर्चा ऐरो नामक जहाज़ को पकड़ लिया तथा उसके 14 नाविकों में से 12 को बंदी बना लिया। यह जहाज एक चीनी व्यापारी का था तथा हांगकांग में पंजीकृत हुआ था। इस जहाज़ पर ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था।
हैरी पार्कस नामक अंग्रेज़ अधिकारी ने चीन की इस कार्यवाही की निंदा की तथा बंदी बनाए गए व्यक्तियों को छोड़ने के लिए कहा। उसने यह भी कहा कि चीनी अधिकारी इस घटना के लिए माफी माँगें तथा भविष्य में ऐसी घटना न होने का आश्वासन दें। चीनी अधिकारियों ने अपनी कार्यवाही को उचित ठहराया तथा अंग्रेजों की माँग मानने से इंकार कर दिया।
इसके पश्चात् अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपनी मांगों के लिए 48 घंटे का समय दिया। चीनी अधिकारियों ने बंदी बनाए गए सभी 12 नाविकों को छोड़ दिया परंतु बाकी माँगें मानने से इंकार कर दिया। चीनियों के इस व्यवहार से अंग्रेज़ रुष्ट हो गए तथा उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया।
प्रश्न 20.
तीनस्तीन की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
तीनस्तीन की संधि पर 26 जून, 1858 ई० को चीन, इंग्लैंड तथा फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थीं
- चीन की 11 नई बंदरगाहों को विदेशी देशों के साथ व्यापार तथा निवास के लिए खोल दिया गया।
- चीनी सरकार ने पश्चिमी देशों को अफ़ीम के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी तथा अफ़ीम के व्यापार को वैध घोषित कर दिया।
- चीन की ‘यांगत्सी’ नदी में पश्चिमी देशों के जहाजों को आने-जाने की अनुमति दे दी गई।
- चीन की सरकार ने यह भी स्वीकार कर लिया कि पश्चिमी देश चीन में अपने राजदूत नियुक्त कर सकेंगे।
- ईसाई धर्म के प्रचारकों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे चीन में स्वतंत्रतापूर्वक घम-फिर कर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल ईसाई बना सकते हैं।
- पश्चिमी शक्तियों के राज्य-क्षेत्रातीत अधिकारों को अधिक विस्तृत और व्यापक कर दिया गया। इसके अनुसार उन्हें चीन में निवास करने और व्यापार करने की सुविधा दी गई।
प्रश्न 21.
आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है ? उसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
अथवा
डॉ० सन-यात-सेन के तीन सिद्धांत क्या थे ?
उत्तर:
डॉ० सन-यात-सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। उसके राजनीतिक विचार तीन सिद्धांतों पर आधारित थे। उनका पहला सिद्धांत ‘राष्ट्रीयता’ का था। डॉ० सन-यात-सेन जानते थे कि चीन में राजनीतिक एकता का पूरी तरह अभाव है। जनता में स्थानीय तथा प्रांतीय भावनाएँ बड़ी प्रबल थीं।
इसी कारण साम्राज्यवादी शक्तियाँ चीन में अपना प्रभाव स्थापित कर रही थीं। अतः डॉ० सन-यात-सेन ने चीन में राष्ट्रीय भावनाएँ जगाने का प्रयत्न किया। राजनीतिक लोकतंत्र’ उनका दूसरा सिद्धांत था। वह चीन में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। लोकतंत्र की सफलता के लिये वह देश की सैनिक शक्ति को दृढ़ बनाना आवश्यक समझते थे।
इसके पश्चात् वह राजनीतिक चेतना का प्रसार करना चाहते थे। अंत में वह लोकतंत्रीय सरकार का निर्माण करना चाहते थे। उनका तीसरा सिद्धांत ‘जनता की आजीविका’ था। आजीविका के प्रश्न को हल करने के लिए वह चीन में भूमि का समान वितरण चाहते थे।
प्रश्न 22.
‘कुओमीनतांग’ से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर:
1905 ई० में डॉ० सन-यात-सेन ने तुंग-मिंग-हुई नामक दल की स्थापना की थी। इस दल की स्थापना जापान में की गई थी। 1911 ई० में चीनी क्रांति के समय यह दल काफी शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में मांचू वंश के साथ जो समझौता किया गया था, उसकी शर्ते भी इस दल के द्वारा तय की गई थीं।
परंतु गणतंत्र की स्थापना के पश्चात् जब युआन शी-काई ने निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया तो डॉ० सन-यात-सेन ने छोटे-छोटे दलों को मिला कर एक नया राष्ट्रीय दल बनाने का निर्णय किया। अत: 1912 ई० में तुंग-मेंग हुई तथा चीन के अन्य दलों को मिलाकर एक नये राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई।
इस दल का नाम कुओमीनतांग रखा गया। जब 1913 ई० में संसद् के चुनाव हुए तो इस दल को काफी सफलता प्राप्त हुई। यह दल युआन-शी-काई के निरंकुश शासन के विरुद्ध था। परिणामस्वरूप युआन-शी-काई से इस दल का संघर्ष आरंभ हो गया।
प्रश्न 23.
1911 ई० की चीनी क्रांति के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करो। .
उत्तर:
1911 ई० की चीनी क्रांति का महत्त्वपूर्ण कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। इससे भोजन की समस्या गंभीर होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त 1910-1911 ई० में भयंकर बाढ़ों के कारण लाखों लोगों की जानें गईं तथा देश में भुखमरी फैल गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप विद्रोह की आग भड़क उठी।
क्राँति का दूसरा कारण ‘प्रवासी चीनियों का योगदान’ था। विदेशों में रहने वाले चीनी लोग काफी धनी हो गए थे। वे चीन में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में थे। अत: उन्होंने क्रांतिकारी संस्थाओं की खूब सहायता की। माँचू सरकार के नये कर भी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुए। इन करों के लगने से चीन में क्रांति की भावनाएँ भड़क उठीं।
जापान की उन्नति भी चीनी क्रांति का एक कारण था। चीन के लोग माँचू सरकार को समाप्त करके जापान की भाँति उन्नति करना चाहते थे। चीन में यातायात के साधनों का सुधार होने के कारण चीनी क्रांति के विचारों के प्रसार को काफी बल मिला। अतः यह भी क्रांति का एक अन्य कारण था।
प्रश्न 24.
1911 ई० की चीनी क्रांति का क्या महत्त्व है ?
उत्तर:
(1) 1911 ई० की क्रांति का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि लगभग तीन सौ वर्षों से स्थापित माँचू शासन का अंत हो गया।
(2) माँचू शासन के अंत के पश्चात् युआन-शी-काई चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना।
(3) 1911 ई० की क्रांति के कारण चीन के शिक्षित नवयुवकों में नवीन विचारों का संचार हुआ। पश्चिमी विचारकों से प्रेरित होकर चीनी लोगों का दृष्टिकोण बदल गया।
(4) राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के पश्चात् चीन धीरे-धीरे आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ।
(5) चीन के लोगों को शताब्दियों से हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार से छुटकारा मिला तथा आत्म-सम्मान की प्राप्ति हुई। निस्संदेह यह क्राँति चीन के इतिहास में एक नया मोड़ सिद्ध हुई।
प्रश्न 25.
चार मई आंदोलन क्या था ?
उत्तर:
1919 ई० में वर्साय पेरिस में हुए शाँति सम्मेलन में चीन को भारी निराशा हाथ लगी। शाँति सम्मेलन के निर्णयों के परिणामस्वरूप चीनी लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्र चीन में जापान के प्रभाव को कम करने में असफल रहे थे। इस कारण चीन के लोग जापान के विरुद्ध हो गए।
इस कारण 4 मई, 1919 ई० में 3000 से अधिक विद्यार्थियों तथा अध्यापकों ने पीकिंग (बीजिंग) के तियानमेन चौक में एक भारी प्रदर्शन किया। उन्होंने वर्साय में शातुंग पर दिए गए निर्णय की घोर आलोचना की। सरकार ने इस भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग से काम लिया। इतिहास में यह घटना ‘चार मई दिवस’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना से चीनी लोगों में एक नई चेतना का संचार हुआ तथा 1949 ई० की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ।
प्रश्न 26.
1949 ई० की चीनी क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
1949 ई० की चीनी क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे
(1) शक्तिशाली केंद्रीय सरकार-1949 ई० की क्राँति से चीन में एकता स्थापित हुई। केवल फारमोसा को छोड़ कर शेष सारा देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन लाया गया। राजनीतिक एकता के साथ-साथ सारे देश में एक प्रकार का ही शासन स्थापित किया गया। अब चीन अयोग्य तथा भ्रष्ट शासन से मुक्त हो चुका था । चीन वासी अब अपने पर गर्व कर सकते थे। इस प्रकार माँचू शासन के अंत के पश्चात् प्रथम बार चीनी लोगों को शक्तिशाली केंद्रीय सरकार मिली।
(2) शाँति एवं सुरक्षा–साम्यवादी सरकार की स्थापना से चीन में काफी समय से व्याप्त अराजकता एवं अव्यवस्था का अंत हुआ तथा पूर्ण स्थायी शाँति की स्थापना हुई। साम्यवादियों ने अपनी कुशल पुलिस व्यवस्था तथा गुप्तचर व्यवस्था से क्राँति का विरोध करने वालों तथा समाज विरोधी तत्त्वों का अंत कर दिया। इससे स्थायी शाँति की स्थापना हुई तथा लोग अपने-आप को सुरक्षित अनुभव करने लगे।
(3) सामाजिक सुधार-साम्यवादी सरकार ने अनेकों सामाजिक सुधार भी किए। उन्होंने समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों का अंत करके महान् कार्य किया। साम्यवादी सरकार ने चीन में अफ़ीम के प्रयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआबाज़ी आदि के विरुद्ध भी कानून बनाए गए। सरकार ने स्त्रियों के उत्थान की ओर भी ध्यान दिया। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। फलस्वरूप उन्हें सदियों पश्चात् चीनी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ।
(4) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव-1949 ई० की चीनी क्राँति से वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया। इस क्राँति से पूर्व छोटे किसानों की दशा बड़ी दयनीय थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के पश्चात् भी उन्हें भर-पेट भोजन नसीब नहीं होता था। इसके विपरीत बड़े-बड़े ज़मींदार विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। 1949 ई० की क्रांति के पश्चात् भूमि का पुनर्विभाजन किया गया। बड़े ज़मींदारों से फालतू भूमि ले कर छोटे किसानों में बाँट दी गई। किसानों की दशा सुधारने के लिए सहकारी समितियाँ भी बनाई गईं।
प्रश्न 27.
माओ-त्सेतुंग के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
माओ-त्सेतुंग को आधुनिक चीन का निर्माता स्वीकार किया गया है। वह किसानों और श्रमिकों का प्रबल समर्थक था। साम्यवाद में उसका दृढ़ विश्वास था। माओ का जन्म 1893 ई० में हूनान प्रांत में स्थित शाओ-शां नामक गाँव में हुआ। उसके पिता का नाम माओ-जेने-शुंग था।माओ को वाशिंगटन, रूसो और नेपोलियन की जीवन गाथाओं ने बहुत प्रभावित किया था।
उसकी सहानुभूति किसानों के साथ थी और उसने उनके लिए काम करने का निश्चय किया। उसने अकाल से भूखी मर रही जनता पर शासकों द्वारा अत्याचार को देखा। 1917 ई० की रूसी क्रांति का युवा माओ पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह उग्र क्रांतिकारी बन गया। उसने लाल सेना का गठन किया। 1930 ई० में वह किसानों और मजदूरों की सभा का सभापति बन गया और भूमिगत होकर काम करने लगा।
उसके सिर पर 25 लाख डालर का ईनाम था। उसने 1934 ई० में लाल सेना की सहायता से च्यांग-काई-शेक की विशाल सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। पाँचवें आक्रमण में उस पर इतना दबाव पड़ा कि उसने ‘महाप्रस्थान’ की योजना बनाई। माओ ने अपना संघर्ष जारी रखा। आखिर 1949 ई० में च्यांग-काई-शेक को चीन से भाग कर फारमोसा में शरण लेनी पड़ी। माओ-त्से-तुंग को चीन की सरकार का अध्यक्ष चुना गया। 1976 ई० में अपनी मृत्यु तक वह इसी पद पर बना रहा।

प्रश्न 28.
लाँग मार्च पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
उत्तर:
लाँग मार्च (लंबी यात्रा) चीन के इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1934 ई० में चियांग-काई-शेक जो कि साम्यवादियों को अपना कट्टर दुश्मन मानता था का विनाश करने के उद्देश्य से कियांग्सी का घेराव कर लिया। राष्ट्रवादी सेना के घेराव के कारण साम्यवादी एक गहन संकट में फंस गए। उन्हें घोर कष्टों को सहन करना पड़ा।
इस घोर संकट के समय में माओ-त्सेतुंग ने बहुत साहस से कार्य लिया। उसने अपने अधीन एक लाख लाल सेना एकत्रित की तथा वह चियांग-काई-शेक के घेराव को तोड़ते हुए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा 16 अक्तूबर, 1934 ई० को आरंभ की गई थी। उसने शांग्सी तक का 6,000 मील का कठिन सफर तय किया। यह एक बहुत जोखिम भरी यात्रा थी।
रास्ते में उन्हें चियांग-काई-शेक की सेना का अनेक बार सामना करना पड़ा। उन्हें भूखे-प्यासे अनेक वनों, नदियों एवं कठिन पर्वतों को पार करना पड़ा। इनके चलते करीब 80 हज़ार माओ के सैनिक रास्ते में मृत्यु का ग्रास बन गए। 370 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात् 20 अक्तूबर, 1935 ई० को माओ-त्सेतुंग अपने 20 हजार सैनिकों के साथ शांग्सी पहुँचने में सफल हुआ। निस्संदेह विश्व इतिहास में इस घटना की कोई उदाहरण नहीं मिलती।
प्रश्न 29.
‘लंबी छलाँग वाला आंदोलन’ से क्या अभिप्राय है ? क्या यह सफल रहा ?
उत्तर:
चीन में लंबी छलाँग वाला आंदोलन 1958 ई० में चलाया गया। इसका उद्देश्य चीन में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीन में कम्यून्स की स्थापना की गई। इनके अपने खेत एवं कारखाने आदि होते थे। प्रत्येक कम्यून उत्पादन, वितरण एवं खपत आदि पर नज़र रखता था।
यद्यपि सरकार द्वारा लगातार इस आंदोलन की सफलता की घोषणा की गई किंतु वास्तविकता यह थी कि यह विफल रहा। लीऊ शाओछी एवं तंग शीयाओफींग नामक नेताओं ने कम्यून प्रथा को बदलने का प्रयास किया क्योंकि ये कुशलता से काम नहीं कर रही थीं। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई थी। दूसरा, कम्यून्स द्वारा तैयार किया गया इस्पात निम्नकोटि का था। तीसरा, रूस से मतभेदों के चलते उसने चीन को आर्थिक सहायता देनी बंद कर दी थी। अतः 1959 ई० में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया।
अति संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न
प्रश्न 1.
प्राचीन चीन का सबसे महानतम इतिहासकार कौन था ?
उत्तर:
प्राचीन चीन का सबसे महानतम इतिहासकार सिमा छियन था।
प्रश्न 2.
नाइतो कोनन कौन था ?
उत्तर:
नाइतो कोनन चीनी इतिहास पर काम करने वाला एक प्रमुख जापानी विद्वान् था। उसने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों एवं अपने पत्रकारिता के अनुभवों का प्रयोग किया। उसने 1907 ई० में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में सहायता की।
प्रश्न 3.
उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है ?
उत्तर:
उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है।
प्रश्न 4.
जापानी लोगों का मुख्य भोजन क्या है ?
उत्तर:
जापानी लोगों का मुख्य भोजन चावल एवं मछली है।
प्रश्न 5.2,228
चीन एवं जापान के कोई दो भौतिक अंतर बताएँ।
उत्तर:
- चीन एक विशाल महाद्वीप है जबकि जापान एक छोटा द्वीप है।
- चीन भूकंप क्षेत्र में नहीं आता जबकि जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं।
प्रश्न 6.
शोगन कौन थे ?
उत्तर:
शोगुन जापान में सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन चलाते थे। वे दैम्यों पर, प्रमुख शहरों एवं खाद्यानों पर नियंत्रण रखते थे। कोई भी व्यक्ति शोगुन की अनुमति के बिना सम्राट से नहीं मिल सकता था। उनके अधीन बड़ी संख्या में सैनिक होते थे।
प्रश्न 7.
सामुराई कौन थे ?
उत्तर:
सामुराई जापान के यौद्धा वर्ग से संबंधित थे। वे शोगुन एवं दैम्यों को प्रशासन चलाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते थे। वे अपनी वफ़ादारी, वीरता एवं सख्त जीवन के लिए प्रसिद्ध थे।
प्रश्न 8.
दैम्यो कौन थे ?
उत्तर:
दैम्यो जापान में अपने अधीन क्षेत्र के मुखिया होते थे। वे अपने क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र होते थे। उन्हें अपने अधीन क्षेत्र के लोगों को मृत्यु दंड देने का अधिकार था। वे सैनिक सेवा करते थे। वे लोक भलाई के कार्य भी करते थे।
प्रश्न 9.
16वीं एवं 17वीं शताब्दी में जापान को एक धनी देश क्यों समझा जाता था ?
उत्तर:
16वीं एवं 17वीं शताब्दी में जापान को एक धनी देश इसलिए समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़े का आयात करता था। जापान इसका मूल्य सोने में चुकाता था। अत: जापान को एक धनी देश समझा जाता था।
प्रश्न 10.
जापान का कौन-सा रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था ?
उत्तर:
जापान का निशिजन रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था।
प्रश्न 11.
जापान में शोगुनों के पतन के लिए उत्तरदायी कोई दो महत्त्वपूर्ण कारण लिखें।
उत्तर:
- शोगुनों की पक्षपातपूर्ण नीति।
- किसानों की दयनीय स्थिति।
प्रश्न 12.
कॉमोडोर मैथ्यू पेरी कौन था ?
उत्तर:
कॉमोडोर मैथ्यू पेरी एक अमरीकी नाविक था। उसे अमरीकी सरकार ने 24 नवंबर, 1852 ई० को जापानी सरकार से बातचीत के लिए भेजा था। वह 3 जुलाई, 1853 ई० को जापान की बंदरगाह योकोहामा पहुँचने में सफल रहा। वह 1854 ई० में जापान सरकार के साथ एक संधि करने में सफल हुआ।
प्रश्न 13.
कॉमोडोर मैथ्यू पेरी की जापान के साथ 1854 ई० में हुई कानागावा संधि की कोई दो शर्ते लिखें।
उत्तर:
- जापान की दो बंदरगाहों शीमोदा एवं हाकोदाटे को अमरीका के जहाजों के लिए खोल दिया गया।
- शीमोदा में अमरीका के वाणिज्य दूत को रहने की अनुमति मिल गई।
प्रश्न 14.
मेज़ी पुनर्स्थापना से क्या भाव है ?
अथवा
मेज़ी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
1868 ई० में जापान में तोकुगावा वंश के शासन का अंत कर दिया गया एवं मुत्सुहितो जापान का नया सम्राट् बना। मुत्सुहितो ने मेज़ी नामक उपाधि को धारण किया। मेज़ी का अर्थ है प्रबुद्ध शासन। जापान के इतिहास में इस घटना को मेज़ी पुनर्स्थापना कहा जाता है।
प्रश्न 15.
मुत्सुहितो जापान का सम्राट् कब बना ? वह इस पद पर कब तक रहा ?
उत्तर:
- मुत्सुहितो जापान का सम्राट् 1868 ई० में बना।
- वह इस पद पर 1912 ई० तक रहा।
प्रश्न 16.
फुकोकु क्योहे से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर:
जापान में मेज़ी काल में सरकार ने फुकोकु क्योहे का नारा दिया। इससे अभिप्राय था समृद्ध देश एवं मज़बूत सेना।
प्रश्न 17.
मेज़ी काल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कोई दो सुधार बताएँ।
उत्तर:
- शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग शिक्षा विभाग की स्थापना की गई।
- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया।
प्रश्न 18.
मेजी काल के कोई दो सैनिक सुधार लिखें।
उत्तर:
- सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया गया।
- 20 वर्ष से अधिक आयु वाले नौजवानों के लिए सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया।
प्रश्न 19.
मेजी काल में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से कौन-से दो पग उठाए गए ?
उत्तर:
- उद्योगों के विकास के लिए यूरोप से मशीनों का आयात किया गया।
- मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया।

प्रश्न 20.
जायबात्सु से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर:
जायबात्सु जापान की बड़ी व्यापारिक संस्थाएँ थीं। इन पर जापान के विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था। इनका प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा।
प्रश्न 21.
मेज़ी संविधान को कब लागू किया गया था ? इसकी कोई दो विशेषताएँ बताएँ।
उत्तर:
- मेज़ी संविधान को 1889 ई० में लागू किया गया था।
- इसमें सम्राट् के अधिकारों की बढ़ौतरी की गई।
- सम्राट् डायट के अधिवेशन को बुला सकता था एवं उसे भंग कर सकता था।
प्रश्न 22.
जापान की प्रथम रेलवे लाइन कब तथा कहाँ बिछाई गई थी ?
उत्तर:
जापान की प्रथम रेलवे लाइन 1870 ई. से 1872 ई० के मध्य तोक्यो एवं योकोहामा के मध्य बिछाई गई थी।
प्रश्न 23.
तनाका शोज़ो कौन था ?
उत्तर:
वह जापान की प्रथम संसद् जिसे डायट कहा जाता था का सदस्य था। उसने 1897 ई० में जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ प्रथम आंदोलन आरंभ किया। उसका कथन था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए।
प्रश्न 24.
मेजी काल में जापानियों की रोजमर्रा जिंदगी में आए महत्त्वपूर्ण बदलाव क्या थे ?
उत्तर:
- इस काल में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा।
- त्पादों के लिए बिजली का प्रचलन बढ़ गया।
- जापानी अब पश्चिमी वेशभूषा पहनने लगे।
प्रश्न 25.
फुकुजावा यूकिची कौन था ?
अथवा
फुकुजावा यूकिची के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
वह मेज़ी काल का एक प्रमुख बुद्धिजीवी था। उसने ‘ज्ञान के लिए प्रोत्साहन’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। उसने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। उसका कथन था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। इससे अभिप्राय था कि जापान को अपने एशियाई लक्षणों को छोड़ कर पश्चिमी लक्षणों को अपनाना चाहिए।
प्रश्न 26.
मियाके सेत्सुरे कौन था ?
उत्तर:
मियाके सेत्सुरे जापान का एक प्रसिद्ध दर्शनशास्त्री था। उसका कथन था कि विश्व सभ्यता के हित में प्रत्येक राष्ट्र को अपने विशेष हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना अपने को विश्व को समर्पित करने के समान है।
प्रश्न 27.
उएकी एमोरी कौन था ?
उत्तर:
उएकी एमोरी जापान में जनवादी अधिकारों के आंदोलन का नेता था। वह चाहता था कि जापान सैन्यवाद की अपेक्षा लोकतंत्र पर बल दे। वह उदारवादी शिक्षा के पक्ष में था। उसका कथन था, “व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है, आज़ादी।” वह फ्रांसीसी क्रांति के मानवों के प्राकृतिक अधिकार एवं जन प्रभुसत्ता का प्रशंसक था।
प्रश्न 28.
1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध के कोई दो कारण बताएँ।
उत्तर:
- रूस की कोरिया में दिलचस्पी।
- कोरिया में तोंगहाक संप्रदाय द्वारा किया गया विद्रोह।
प्रश्न 29.
1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ ? इस संधि की कोई दो धाराएँ लिखो।
उत्तर:
- 1894-95 ई० के चीन-जापान युद्ध का अंत शिमोनोसेकी की संधि द्वारा हुआ।
- चीन ने जापान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी।
- चीन ने माना कि वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जापान को 2 करोड़ तायल देगा।
प्रश्न 30.
1894-95 ई० के चीन-जापान यद्ध के कोई दो परिणाम लिखें।
उत्तर:
- इसमें चीन को पराजय का सामना करना पड़ा।
- इसमें जापान की विजय से उसके सम्मान में बहुत वृद्धि हुई।
प्रश्न 31.
रूस-जापान युद्ध कब हुआ ? इसमें कौन विजयी रहा ?
उत्तर:
- रूस-जापान युद्ध 1904-05 ई० में हुआ।
- इसमें जापान विजयी रहा।
प्रश्न 32.
1904-05 ई० के रूस-जापान युद्ध के कोई दो कारण लिखें।
उत्तर:
- लियाओतुंग पर रूस ने कब्जा कर लिया था।
- मँचूरिया पर रूस एवं जापान कब्जा करना चाहते थे।
प्रश्न 33.
पोर्टसमाउथ की संधि कब हुई ? इस संधि की कोई दो शर्ते लिखें।
उत्तर:
- पोर्टसमाउथ की संधि 1905 ई० में हुई।
- पोर्ट आर्थर एवं लियाओतुंग प्रायद्वीप जापान को मिल गए।
- जापान को स्खालिन द्वीप का दक्षिण भाग प्राप्त हुआ।
प्रश्न 34.
1904-05 ई० के रूस-जापान युद्ध के कोई दो प्रभाव लिखें।
उत्तर:
- इस युद्ध में पराजय के कारण रूस की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा।
- इस विजय से जापान को अन्य क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए एक नया प्रोत्साहन मिला।
प्रश्न 35.
जापान में सैन्यवाद के उदय के कोई दो कारण बताएँ।
उत्तर:
- जापान के सैन्यवादी बहुत महत्त्वाकांक्षी हो गए थे।
- जापानी नवयुवक जापानी सैन्यवाद में विश्वास करते थे।
प्रश्न 36.
जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमरीका ने कब तथा किन दो शहरों पर एटम बम गिराये थे ?
उत्तर:
जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 ई० में अमरीका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराए थे।
प्रश्न 37:
अमरीका ने जापान पर कब-से-कब तक कब्जा किया ? इस समय दौरान जापान पर किसने शासन किया ?
उत्तर:
- अमरीका ने जापान पर 1945 ई० से 1952 ई० तक शासन किया।
- इस समय के दौरान जापान पर जनरल दगलस मेकार्थर ने शासन किया।
प्रश्न 38.
जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले चुनाव कब हुए ? इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता क्या थी ?
उत्तर:
- जापान में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पहले चुनाव 1947 ई० में हुए।
- इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें स्त्रियों को प्रथम बार मतदान करने का अधिकार दिया गया।

प्रश्न 39.
अमरीका ने जापान में कौन-से चार महत्त्वपूर्ण सुधार किए ?
उत्तर:
- उसने जापान में 1947 ई० में एक नया संविधान लागू किया।
- उसने जापान में भारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया।
- उसने जापान में आधुनिक शिक्षा को लागू किया।
- उसने जापान का निरस्त्रीकरण किया।
प्रश्न 40.
जापान में कब तथा कहाँ प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था.?
उत्तर:
जापान में 1964 ई० में तोक्यो में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
प्रश्न 41.
प्रथम अफ़ीम युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ ? इसमें कौन-विजयी रहा ?
उत्तर:
- प्रथम अफ़ीम युद्ध 1839 ई० से 1842 ई० को इंग्लैंड एवं चीन के मध्य हुआ।
- इसमें इंग्लैंड की विजय हुई।
प्रश्न 42.
प्रथम अफ़ीम युद्ध के कोई दो कारण लिखें।
उत्तर:
- चीनियों द्वारा यूरोपियों से किया जाने वाला घृणापूर्ण व्यवहार।
- चीन के सम्राट् द्वारा कमिश्नर लिन की नियुक्ति।
प्रश्न 43.
प्रथम अफ़ीम युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ ? यह संधि कब हुई थी ?
उत्तर:
- प्रथम अफ़ीम युद्ध नानकिंग की संधि के साथ समाप्त हुआ था।
- यह संधि 1842 ई० को हुई थी।
प्रश्न 44.
नानकिंग की संधि की कोई दो शर्ते लिखें।
उत्तर:
- हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को सौंपा गया।
- ब्रिटेन के लिए पाँच चीनी बंदरगाहें व्यापार के लिए खोल दी गईं।
प्रश्न 45.
प्रथम अफ़ीम युद्ध के कोई दो प्रभाव लिखें।
उत्तर:
- इस युद्ध में पराजय के कारण चीन के सम्मान को गहरा आघात लगा।
- इससे चीन की आर्थिक समस्याएँ बढ़ गईं।
प्रश्न 46.
चीन में ताइपिंग विद्रोह कब हुआ ? इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था ?
उत्तर:
- चीन में ताइपिंग विद्रोह 1850-1864 ई० में हुआ था।
- इसका उद्देश्य चीन में मिंग शासन की पुनः स्थापना करना था।
प्रश्न 47.
चीन एवं ब्रिटेन के मध्य द्वितीय अफ़ीम युद्ध कब हुआ ? इसमें कौन विजयी रहा ?
उत्तर:
- चीन एवं ब्रिटेन के मध्य द्वितीय अफ़ीम युद्ध 1856 ई० से 1860 ई० के मध्य लड़ा गया।
- इसमें ब्रिटेन विजयी रहा।
प्रश्न 48.
चीन एवं ब्रिटेन के मध्य तीनस्तीन की संधि कब हुई ?
उत्तर:
चीन एवं ब्रिटेन के मध्य तीनस्तीन की संधि 1858 ई० में हुई।
प्रश्न 49.
रिवाइव चाइना सोसायटी की स्थापना कब तथा किसने की थी ?
उत्तर:
रिवाइव चाइना सोसायटी की स्थापना 1894 ई० में डॉक्टर सन-यात-सेन ने की थी।
प्रश्न 50.
रिवाइव चाइना सोसायटी के कोई दो प्रमुख उद्देश्य लिखें।
उत्तर:
- चीन से माँचू शासन का अंत करना।
- चीनी समाज का पुनः निर्माण करना।
प्रश्न 51.
डॉक्टर सन-यात-सेन ने तुंग-मिंग-हुई की स्थापना कब की ? इसका उद्देश्य क्या था ?
उत्तर:
- डॉक्टर सन-यात-सेन ने तुंग-मिंग-हुई की स्थापना 1905 ई० में की।
- इसका उद्देश्य चीन में क्रांति करना था।
प्रश्न 52.
डॉक्टर सन-यात-सेन ने किन तीन सिद्धांतों का प्रचलन किया था ?
उत्तर:
डॉक्टर सन-यात-सेन ने राष्ट्रवाद, गणतंत्र एवं समाजवाद नामक तीन सिद्धांतों का प्रचलन किया।
प्रश्न 53.
1911 ई० की चीनी क्रांति के कोई दो कारण लिखें।
उत्तर:
- चीन में बढ़ती हुई समस्याएँ।
- डॉक्टर सन-यात-सेन का योगदान।
प्रश्न 54.
1911 ई० की चीनी क्रांति के कोई दो परिणाम बताएँ ।
उत्तर:
- इसने चीन में माँचू वंश का अंत कर दिया।
- चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई।

प्रश्न 55.
चीन में माँचू वंश का अंत कब हुआ एवं गणतंत्र की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई ?
उत्तर:
- चीन में माँचू वंश का अंत 1917 ई० में हुआ।
- चीन में गणतंत्र की स्थापना डॉक्टर सन-यात-सेन के नेतृत्व में हुई।
प्रश्न 56.
चीन में कुओमीनतांग की स्थापना किसने तथा कब की ?
उत्तर:
चीन में कुओमीनतांग की स्थापना डॉक्टर सन-यात-सेन ने 1912 ई० में की।
प्रश्न 57.
चीन में कुओमीनतांग दल के कोई दो उद्देश्य लिखें।
उत्तर:
- चीन में शाँति स्थापित करना।
- चीनी सेना में कड़ा अनुशासन लागू करना।
प्रश्न 58.
4 मई आंदोलन कब तथा कहाँ हुआ था ?
उत्तर:
4 मई आंदोलन 1919 ई० में बीजिंग में हुआ था।
प्रश्न 59.
माओ-त्सेतुंग के जीवन पर संक्षिप्त नोट लिखो।
उत्तर:
माओ-त्सेतुंग का जन्म 1893 ई० में चीन के हूनान प्रांत में स्थित शाओ-शां नामक गाँव में हुआ। उसने 1934-35 ई० में लाँग मार्च का नेतृत्व किया। माओ-त्सेतुंग ने नया लोकतंत्र नामक पुस्तक 1940 ई० में लिखी। उसके नेतृत्व में 1949 ई० की क्राँति हुई।
प्रश्न 60.
माओ-त्सेतुंग ने कौन-सी प्रसिद्ध पुस्तक तथा कब लिखी ?
उत्तर:
माओ-त्सेतुंग ने नया लोकतंत्र नामक पुस्तक 1940 ई० में लिखी।
प्रश्न 61.
लाँग मार्च से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर:
साम्यवादियों द्वारा की गई नाकेबंदी के कारण माओ-त्सेतुंग ने 1934-35 ई० में लाँग मार्च का नेतृत्व किया। यह 6000 मील का लंबा सफर था। इस सफर के दौरान लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।
प्रश्न 62.
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की सरकार कब तथा किसके नेतृत्व में स्थापित हुई ?
उत्तर:
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की सरकार 1949 ई० में माओ-त्सेतुंग के नेतृत्व में स्थापित हुई।
प्रश्न 63.
चीन में लंबी छलाँग की घोषणा कब की गई थी ? इसका उद्देश्य क्या था ?
उत्तर:
- चीन में लंबी छलाँग की घोषणा 1958 ई० में की गई थी।
- इसका उद्देश्य चीन के उद्योगों को प्रोत्साहन देना था।
प्रश्न 64.
महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्राँति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर:
महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्राँति को चीन में माओ-त्सेतुंग द्वारा 1966 ई० में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य चीन में प्राचीन संस्कृति को पुनः स्थापित करना एवं माओ-त्सेतुंग के विरोधियों के विरुद्ध अभियान छेड़ना था।
प्रश्न 65.
चीन में आधुनिकीकरण के लिए कब तथा किसने चार सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की ? ये चार सूत्र कौन-से थे ?
उत्तर:
- चीन में आधुनिकीकरण के लिए 1978 ई० में तंग शीयाओफींग ने चार सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की।
- ये चार सूत्र थे-विज्ञान, उद्योग, कृषि एवं रक्षा।
प्रश्न 66.
चियांग-काई-शेक ने ताइवान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कौन-से दो मुख्य सुधार किए ?
उत्तर:
- उसने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की।
- उसने उद्योगों के विकास पर बल दिया।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न 1.
प्राचीन चीन का सबसे महान् इतिहासकार किसे माना जाता है ?
उत्तर:
सिमा छियन को।
प्रश्न 2.
मैटियो रिक्की कौन थे ?
उत्तर:
चीन में एक जेसूइट पादरी।
प्रश्न 3.
नाइतो कोनन कौन थे ?
उत्तर:
एक प्रसिद्ध जापानी विद्वान्।
प्रश्न 4.
जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है ?
उत्तर:
होशू।
प्रश्न 5.
जापान की राजधानी तोक्यो को पहले किस नाम से जाना जाता था ?
उत्तर:
एदो।
प्रश्न 6.
जापान का प्रथम सम्राट् किसे माना जाता है ?
उत्तर:
जिम्मू।
प्रश्न 7.
उगते हुए सूर्य का देश किसे माना जाता है ?
उत्तर:
जापान को।
प्रश्न 8.
जापान की प्रसिद्ध मछली कौन-सी है ?
उत्तर:
साशिमी।
प्रश्न 9.
जापान में सम्राट् किस नाम से जाने जाते थे ?
उत्तर:
मिकाडो।
प्रश्न 10.
शोगुनों के उत्थान से पूर्व जापानी सम्राट् कहाँ से शासन करते थे ?
उत्तर:
क्योतो।
प्रश्न 11.
जापान में तोकुगावा कब सत्ता में आए ?
उत्तर:
1603 ई० में।
प्रश्न 12.
सामुराई कौन थे ?
उत्तर:
योद्धा वर्ग।

प्रश्न 13.
17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में दुनिया में सबगे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था।
उत्तर:
एदो।
प्रश्न 14.
16वीं शताब्दी में निशिजन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था ?
उत्तर:
रेशम।
प्रश्न 15.
जापान में शोगुन पद का अं का हुआ ?
उत्तर:
1867 ई० में।
प्रश्न 16.
अमरीका का कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जापान कब पहुँचा ?
उत्तर:
1853 ई० में।
प्रश्न 17.
जापान एवं अमरीका के मध्य कानागावा की संधि कब हुई ?
उत्तर:
1854 ई० में।
प्रश्न 18.
मुत्सुहितो जापान का सम्राट् कब बना ?
उत्तर:
1868 ई० में।
प्रश्न 19.
मुत्सुहितो ने किसे जापान की राजधानी बनाया ?
उत्तर:
तोक्यो।
प्रश्न 20.
जापान में सामंती प्रथा के अंत की घोषणा कब की गई ?
उत्तर:
1871 ई० में।
प्रश्न 21.
जापान में तोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी ?
उत्तर:
1877 ई० में।
प्रश्न 22.
दि टेल ऑफ़ दि गेंजी का लेखक कौन था ?
उत्तर:
मुरासाकी शिकिबु।
प्रश्न 23.
फुकोकु क्योहे से क्या अभिप्राय था ?
उत्तर:
समूह देश एवं मज़बूत सेना।
प्रश्न 24.
जापान में विशिष्ट एवं धनी परिवार क्या कहलाते थे ?
उत्तर:
जायबात्सु।
प्रश्न 25.
1897 ई० में जापान में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध किसने प्रथम जन आंदोलन का नेतृत्व किया था ?
उत्तर:
तनाका शोज़ो ने।
प्रश्न 26.
जापान में प्रथम आधुनिक हड़ताल कब हुई ?
उत्तर:
1886 ई० में।
प्रश्न 27.
जापान में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई ?
उत्तर:
तोक्यो एवं योकोहामा।
प्रश्न 28.
बैंक ऑफ़ जापान को कब खोला गया था ?
उत्तर:
1882 ई० में।
प्रश्न 29.
मेज़ी संविधान को कब लागू किया गया था ?
उत्तर:
1889 ई० में।
प्रश्न 30.
जापान में प्रथम रेडियो स्टेशन कब खुला ?
उत्तर:
1925 ई० में।
प्रश्न 31.
जापान में जनवादी अधिकारों के आंदोलन का नेता कौन था ?
उत्तर:
उएकी एमोरी।
प्रश्न 32.
‘एक गुड़िया का घर’ नामक प्रसिद्ध नाटक का लेखक कौन था ?
उत्तर:
इब्सन।
प्रश्न 33.
चीन-जापान युद्ध कब हुआ ?
उत्तर:
1894-95 ई० में।
प्रश्न 34.
चीन-जापान के मध्य शिमोनोसेकी की संधि कब हुई ?
उत्तर:
1895 ई० में।
प्रश्न 35.
रूस एवं जापान के मध्य युद्ध कब हुआ ?
उत्तर:
1904-05 ई० में।
प्रश्न 36.
संयुक्त राज्य अमरीका ने जापान के किस शहर पर 6 अगस्त, 1945 ई० को प्रथम परमाणु बम गिराया ?
उत्तर:
हिरोशिमा पर।
प्रश्न 37.
जापान पर अमरीका का कब्जा कब से लेकर कब तक रहा ?
उत्तर:
1945 ई० से लेकर 1952 ई० तक।
प्रश्न 38.
तोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया ?
उत्तर:
1964 ई० में।
प्रश्न 39.
जापान में बुलेट ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है ?
उत्तर:
शिंकासेन।
प्रश्न 40.
जापान में नागरिक समाज आंदोलन का विकास कब हुआ ?
उत्तर:
1960 के दशक में।
प्रश्न 41.
चीन में पीली नदीको किस नाम से जाना जाता है ?
उत्तर:
हवांग हो।

प्रश्न 42.
चीन की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है ?
उत्तर:
यांग्त्सी नदी।
प्रश्न 43.
चीन के सबसे प्रमुख जातीय समूह का नाम क्या है ?
उत्तर:
हान।
प्रश्न 44.
चीन का सबसे प्रसिद्ध खाना क्या कहलाता है ?
उत्तर:
डिम सम।
प्रश्न 45.
पहला अफ़ीम युद्ध कब हुआ ?
उत्तर:
1839-1842 ई०
प्रश्न 46.
पहला अफ़ीम युद्ध किनके मध्य हुआ ?
उत्तर:
इंग्लैंड एवं चीन।
प्रश्न 47.
नानकिंग की संधि कब हुई ?
उत्तर:
1842 ई० में।
प्रश्न 48.
द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ ?
उत्तर:
1856-60 ई०।
प्रश्न 49.
तीनस्तीन की संधि कब हुई ?
उत्तर:
1858 ई० में।
प्रश्न 50.
आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है ?
उत्तर:
डॉ० सन-यात-सेन को।
प्रश्न 51.
डॉ० सन-यात-सेन ने कितने सिद्धांतों का प्रचलन किया ?
उत्तर:
तीन।
प्रश्न 52.
डॉ० सन-यात-सेन ने तुंग मिंग हुई की स्थापना कब की ?
उत्तर:
1905 ई० में।
प्रश्न 53.
सन-यात-सेन की मृत्यु कब हुई ?
उत्तर:
1925 ई० में।
प्रश्न 54.
पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ?
उत्तर:
1902 ई० में।
प्रश्न 55.
चीनी क्रांति कब हुई ?
उत्तर:
1911 ई० में।
प्रश्न 56.
चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना ?
उत्तर:
युआन-शी-काई।
प्रश्न 57.
चीन में कुओमीनतांग दल की स्थापना कब हुई ?
उत्तर:
1921 ई० में।
प्रश्न 58.
4 मई, 1919 ई० का आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ ?
उत्तर:
पीकिंग।
प्रश्न 59.
जापान ने चीन पर आक्रमण कब किया ?
उत्तर:
1 जुलाई, 1937 ई०।
प्रश्न 60.
चीन में लांग मार्च का नेतृत्व किसने किया ?
उत्तर:
माओ-त्सेतुंग।
प्रश्न 61.
‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की स्थापना कब हुई ?
उत्तर:
1 अक्तूबर, 1919 ई०।
प्रश्न 62.
गणराज्यी चीन का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ?
उत्तर:
माओ-त्सेतुंग को।
प्रश्न 63.
गणराज्यी चीन का प्रथम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया ?
उत्तर:
चाऊ एनलाई को।
प्रश्न 64.
पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना की स्थापना कब की गई ?
उत्तर:
1950 ई० में।
प्रश्न 65.
1958 ई० में चीन में कौन-सा आंदोलन चलाया गया ?
उत्तर:
लंबी छलाँग वाला आंदोलन।
प्रश्न 66.
तंग शीयाओफींग चीन में कब सत्ता में आया ?
उत्तर:
1976 ई० में।
प्रश्न 67.
चीन में चार आधुनिकीकरणों की घोषणा कब की गई थी ?
उत्तर:
1978 ई० में।
प्रश्न 68.
ताइवान को पहले किस नाम से जाना जाता था ?
उत्तर:
फारमोसा।
प्रश्न 69.
ताइवान की राजधानी किसे घोषित किया गया ?
उत्तर:
ताइपेइ को।
प्रश्न 70.
चियांग-काई-शेक की मृत्यु कब हुई ?
उत्तर:
1975 ई० में।
प्रश्न 71.
ताइवान में मार्शल लॉ के अंत की घोषणा कब की गई ?
उत्तर:
1987 ई० में।
रिक्त स्थान भरिए
1. 1603 ई० में जापान में ……………… वंश की स्थापना हुई।
उत्तर:
तोकुगावा
2. मेजी पुनर्स्थापना ……………….. ई० में हुई।
उत्तर:
1868
3. ……………….. ई० में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य किया गया।
उत्तर:
1870

4. जापान की पहली रेल लाइन ……………….. ई० में बिछाई गई।
उत्तर:
1870
5. जापान में ……………….. ई० में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ था।
उत्तर:
1872
6. जापान में सर्वप्रथम महिलाओं द्वारा आधुनिक हड़तालों का आयोजन ……………….. ई० में हुआ था।
उत्तर:
1886
7. जापान में औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध पहला आंदोलन ………………. ई० में आरंभ किया गया।
उत्तर:
1897
8. जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ़ प्रथम आंदोलन …………… द्वारा आरंभ किया गया।
उत्तर:
तनाको शोज़ो
9. ‘ज्ञान के लिए प्रोत्साहन’ नामक पुस्तक की रचना जापान के महान् बुद्धिजीवी ……………… द्वारा की गई __ थी।
उत्तर:
फुकुज़ावा यूकिची
10. ‘एक गुड़िया का घर’ नामक नाटक की रचना ……………….. द्वारा की गई थी।
उत्तर:
इबसन
11. जापान में प्रथम बार ……………….. ई० में चुनाव हुए। .
उत्तर:
1946
12. जापान में ……………….. ई० में बुलेट ट्रेन चलाई गई।
उत्तर:
1964
13. जापान में प्रथम अफ़ीम युद्ध ……………….. ई० में हुआ।
उत्तर:
1839
14. दूसरा अफ़ीम युद्ध ……………… ई० में हुआ।
उत्तर:
1856
15. मांचू साम्राज्य का अंत ………………. ई० में किया गया।
उत्तर:
1911
16. आधुनिक चीन का संस्थापक ………………. को माना जाता है।
उत्तर:
सन-यात-सेन
17. कुओमिनतांग का नेता ……………….. था।
उत्तर:
चियांग काइशेक
18. पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना ……………….. ई० में की गई।
उत्तर:
1902
19. 1945 ई० में ……………….. तथा ……………….. पर बम फेंके गए।
उत्तर:
नागासाकी, हिरोशिमा
20. चीन में साम्यवादी की स्थापना ……………… ई० में हुई।
उत्तर:
1921
21. ……………… ई० में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृहयुद्ध में विजय प्राप्त की।
उत्तर:
1949
22. जापान व आंग्ल अमेरिका में ……………….. ई० में भयंकर युद्ध हुआ।
उत्तर:
1945
23. जापान का आधुनिकीकरण का सफर ……………… के सिद्धान्तों पर आधारित था।
उत्तर:
पूँजीवाद
24. ……………….. को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है।
उत्तर:
सिमा छियन
25. 1907 ई० में जापान में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में ……………….. ने सर्वाधिक सहायता की।
उत्तर:
नाइतो कोनन
26. जापान द्वारा चीन से ……………… का आयात किया जाता था
उत्तर:
रेशम
27. जापान द्वारा भारत से ……………….. का आयात किया जाता था।
उत्तर:
कपड़ा
28. ……………… ई० में विदेशी व्यापार होना आरंभ हुआ था।
उत्तर:
1859
29. ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ की सरकार ……………….. में कायम हुई।
उत्तर:
1949 ई०
30. चीन की पोट्सडैम उद्घोषणा ………….. ई० में की गई।
उत्तर:
1949
बहु-विकल्पीय प्रश्न
1. ‘नाइतो कोनन’ किस देश के रहने वाले थे ?
(क) चीन
(ख) जापान
(ग) कनाडा
(घ) ऑस्ट्रेलिया।
उत्तर:
(ख) जापान
2. निम्नलिखित में से कौन-सा द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ?
(क) होंशू
(ख) क्यूशू
(ग) शिकोकू
(घ) होकाइदो।
उत्तर:
(क) होंशू
3. ‘उगते हुए सूर्य का देश’ किसे कहा जाता है ?
(क) इंडोनेशिया
(ख) जापान
(ग) कनाडा
(घ) इंग्लैंड।
उत्तर:
(ख) जापान
4. कुमे कुनीताके किस देश के रहने वाले थे ?
(क) चीन
(ख) जापान
(ग) इंग्लैंड
(घ) फ्राँस।
उत्तर:
(ख) जापान
5. एदो किस शहर का पुराना नाम है ?
(क) पेरिस
(ख) टोकियो
(ग) सिडनी
(घ) लंदन।
उत्तर:
(ख) टोकियो
6. जापान में शोगुनों ने सत्ता को कब हथिया लिया था ?
(क) 1192 ई०
(ख) 1503 ई०
(ग) 1603 ई०
(घ) 1867 ई०।
उत्तर:
(क) 1192 ई०

7. जापान में तोकगावा कब से लेकर कब तक सत्ता में रहे ?
(क) 1192 ई० से 1203 ई० तक
(ख) 1203 ई० से 1603 ई० तक
(ग) 1603 ई० से 1867 ई० तक
(घ) 1867 ई० से 1971 ई० तक।
उत्तर:
(ग) 1603 ई० से 1867 ई० तक
8. तोकुगावा शासनकाल में जापान की राजधानी कौन-सी थी ?
(क) ओसाका
(ख) एदो
(ग) क्योतो
(घ) तोक्यो।
उत्तर:
(ख) एदो
9. कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जापान कब पहुँचा ?
(क) 1851 ई० में
(ख) 1852 ई० में
(ग) 1853 ई० में
(घ) 1854 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1853 ई० में
10. जापान में मेज़ी पुनस्र्थापना कब हुई ?
(क) 1853 ई० में
(ख) 1854 ई० में
(ग) 1868 ई० में
(घ) 1878 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1868 ई० में
11. जापान में मुत्सुहितो का शासनकाल क्या था ?
(क) 1192 ई० से 1603 ई० तक
(ख) 1603 ई० से 1867 ई० तक
(ग) 1868 ई० से 1902 ई० तक
(घ) 1868 ई० से 1912 ई० तक।
उत्तर:
(घ) 1868 ई० से 1912 ई० तक।
12. मेज़ी शासनकाल में किसे जापान की राजधानी घोषित किया गया ?
(क) एदो
(ख) तोक्यो
(ग) नागासाकी
(घ) क्योतो।
उत्तर:
(ख) तोक्यो
13. जापान में तोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ?
(क) 1871 ई० में
(ख) 1875 ई० में
(ग) 1877 ई० में
(घ) 1901 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1877 ई० में
14. जापान में सैनिक सेवा को कब अनिवार्य बनाया गया था ? ।
(क) 1872 ई० में
(ख) 1876 ई० में
(ग) 1877 ई० में
(घ) 1879 ई० में।
उत्तर:
(क) 1872 ई० में
15. जापान में किसने औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध प्रथम जन आंदोलन का नेतृत्व किया ?
(क) मुत्सुहितो
(ख) कुमो कुनीताके
(ग) तनाका शोज़ो
(घ) नाइतो कोनन।
उत्तर:
(ग) तनाका शोज़ो
16. जापान की पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी ?
(क) 1707-09
(ख) 1763-65
(ग) 1830-32
(घ) 1870-72
उत्तर:
(घ) 1870-72
17. बैंक ऑफ़ जापान की स्थापना कब की गई थी ?
(क) 1872 ई० में
(ख) 1875 ई० में
(ग) 1879 ई० में
(घ) 1882 ई० में।
उत्तर:
(घ) 1882 ई० में।
18. मेज़ी संविधान कब लागू किया गया था ?
(क) 1869 ई० में
(ख) 1879 ई० में
(ग) 1889 ई० में
(घ) 1892 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1889 ई० में
19. फुकुज़ावा यूकिची कौन था ?
(क) जापान का एक बुद्धिजीवी
(ख) चीन का एक बुद्धिजीवी
(ग) जापान का एक दर्शनशास्त्री
(घ) जापान का एक अधिकारी।
उत्तर:
(क) जापान का एक बुद्धिजीवी
20. जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला ?
(क) 1855 ई० में
(ख) 1885 ई० में
(ग) 1915 ई० में
(घ) 1925 ई० में।
उत्तर:
(घ) 1925 ई० में।
21. चीन-जापान युद्ध कब आरंभ हुआ ?
(क) 1892 ई० में
(ख) 1893 ई० में
(ग) 1894 ई० में
(घ) 1895 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1894 ई० में
22. 1894-95 ई० का चीन-जापान युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ ?
(क) शिमनोसेकी की संधि
(ख) नानकिंग की संधि
(ग) बोग की संधि
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर:
(क) शिमनोसेकी की संधि
23. रूस-जापान युद्ध कब हुआ था ?
(क) 1905 ई० में
(ख) 1907 ई० में
(ग) 1909 ई० में
(घ) 1911 ई० में।
उत्तर:
(क) 1905 ई० में
24. जापान में ‘बुलेट ट्रेन’ की शुरुआत कब हुई ?
(क) 1954 ई० में
(ख) 1964 ई० में
(ग) 1974 ई० में
(घ) 1984 ई० में।
उत्तर:
(ख) 1964 ई० में
25. संयुक्त राज्य अमरीका ने 6 अगस्त, 1945 ई० को जापान के किस शहर पर परमाणु बम फेंका ?
(क) नागासाकी
(ख) हिरोशिमा
(ग) तोक्यो
(घ) ओसाका।
उत्तर:
(ख) हिरोशिमा

26. तोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था ?
(क) 1960 ई० में
(ख) 1962 ई० में
(ग) 1964 ई० में
(घ) 1965 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1964 ई० में
27. निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का दुःख कहा जाता है ?
(क) पर्ल नदी को
(ख) पीली नदी को
(ग) यांगत्सी नदी को
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(ख) पीली नदी को
28. प्रथम अफ़ीम युद्ध किनके मध्य हुआ ?
(क) चीन एवं जापान
(ख) इंग्लैंड एवं जापान
(ग) जापान एवं रूस
(घ) चीन एवं फ्राँस।
उत्तर:
(ख) इंग्लैंड एवं जापान
29. प्रथम अफ़ीम युद्ध कब लड़ा गया था ?
(क) 1803-05 ई० में
(ख) 1839-42 ई० में
(ग) 1856-59 ई० में
(घ) 1876-79 ई० में।
उत्तर:
(ख) 1839-42 ई० में
30. नानकिंग की संधि कब हुई ?
(क) 1839 ई० में
(ख) 1842 ई० में
(ग) 1845 ई० में
(घ) 1849 ई० में।
उत्तर:
(ख) 1842 ई० में
31. द्वितीय अफ़ीम युद्ध कब आरंभ हुआ ?
(क) 1854 ई० में
(ख) 1855 ई० में
(ग) 1856 ई० में
(घ) 1860 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1856 ई० में
32. 1858 ई० को चीन एवं इंग्लैंड के मध्य कौन-सी संधि हुई ?
(क) तीनस्तीन की संधि
(ख) बोग की संधि
(ग) नानकिंग की संधि
(घ) पीकिंग की संधि ।
उत्तर:
(क) तीनस्तीन की संधि
33. बॉक्सर विद्रोह किस देश में हुआ ?
(क) जापान में
(ख) चीन में
(ग) फ्रांस में
(घ) इंग्लैंड में।
उत्तर:
(ख) चीन में
34. चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था ?
(क) 1890 ई० में
(ख) 1895 ई० में
(ग) 1900 ई० में
(घ) 1910 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1900 ई० में
35. ‘सौ दिन के सुधार’ का संबंध किस देश से है ?
(क) चीन
(ख) जापान
(ग) अमरीका
(घ) भारत।
उत्तर:
(क) चीन
36. तुंग-मिंग-हुई की स्थापना कब की गई थी ?
(क) 1902 ई० में
(ख) 1905 ई० में
(ग) 1907 ई० में
(घ) 1911 ई० में।
उत्तर:
(ख) 1905 ई० में
37. सन-यात-सेन ने कितने सिद्धांतों का प्रचलन किया था ?
(क) दो
(ख) तीन
(ग) चार
(घ) पाँच।
उत्तर:
(ख) तीन
38. 1911 ई० की चीनी क्रांति का नेता कौन था?
(क) लियांग किचाऊ
(ख) कंफ्यूशियस
(ग) युआन-शि-काई
(घ) डॉ० सन-यात-सेन।
उत्तर:
(घ) डॉ० सन-यात-सेन।
39. चीन में माँच वंश का अंत कब हुआ ?
(क) 1905 ई० में
(ख) 1909 ई० में
(ग) 1911 ई० में
(घ) 1912 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1911 ई० में
40. आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है ?
(क) कांग यूवेई
(ख) लियांग किचाउ
(ग) सन-यात-सेन
(घ) चियांग-काई-शेक ।
उत्तर:
(ग) सन-यात-सेन
41. पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
(क) 1892 ई० में
(ख) 1902 ई० में
(ग) 1906 ई० में
(घ) 1920 ई० में।
उत्तर:
(ख) 1902 ई० में
42. चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना ?
(क) सन-यात-सेन
(ख) माओ-त्सेतुंग
(ग) युआन-शि-काई
(घ) शाओ तोआफ़ेन !
उत्तर:
(ग) युआन-शि-काई

43. चीन में कुओमीनतांग दल की स्थापना कब की गई थी ?
(क) 1911 ई० में
(ख) 1912 ई० में
(ग) 1921 ई० में
(घ) 1922 ई० में।
उत्तर:
(ख) 1912 ई० में
44. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी ?
(क) 1912 ई० में
(ख) 1920 ई० में
(ग) 1921 ई० में
(घ) 1931 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1921 ई० में
45. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की सरकार का गठन कब हुआ ?
(क) 1911 ई० में
(ख) 1945 ई० में
(ग) 1949 ई० में
(घ) 1951 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1949 ई० में
46. चीन में लाँग मार्च कब आरंभ हुआ था ?
(क) 1911 ई० में
(ख) 1924 ई० में
(ग) 1934 ई० में
(घ) 1935 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1934 ई० में
47. माओ-त्सेतुंग ने चीन में नया संविधान कब लागू किया ?
(क) 1949 ई० में
(ख) 1950 ई० में
(ग) 1951 ई० में
(घ) 1954 ई० में।
उत्तर:
(घ) 1954 ई० में।
48. चीन में लंबी छलाँग वाला आंदोलन कब चलाया गया ?
(क) 1954 ई० में
(ख) 1956 ई० में
(ग) 1958 ई० में
(घ) 1962 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1958 ई० में
49. निम्नलिखित में से किस नेता ने नया लोकतंत्र नामक पुस्तक की रचना की ?
(क) माओ-त्सेतुंग
(ख) चियांग-काई-शेक
(ग) कुमे कुनीताके
(घ) मैटियो रिक्की।
उत्तर:
(क) माओ-त्सेतुंग
50. चीन में महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ कब हुआ ?
(क) 1958 ई० में
(ख) 1962 ई० में
(ग) 1965 ई० में
(घ) 1966 ई० में।
उत्तर:
(घ) 1966 ई० में।
51. चीन में चार आधुनिकीकरणों की घोषणा कब की गई?
(क) 1968 ई० में
(ख) 1976 ई० में
(ग) 1978 ई० में
(घ) 1928 ई० में।
उत्तर:
(ग) 1978 ई० में
52. ताइवान का पहला नाम क्या था ?
(क) फारमोसा
(ख) नानकिंग
(ग) शीमोदा
(घ) हाकोदारे।
उत्तर:
(क) फारमोसा
आधुनिकीकरण के रास्ते HBSE 11th Class History Notes
→ 19वीं शताब्दी में दूर पूर्व एशिया के दो देशों जापान एवं चीन ने आधुनिकीकरण के रास्ते को अपनाया। निस्संदेह दोनों देशों के लिए एक नए युग का सूत्रपात था। जापान प्रशांत महासागर में स्थित कई द्वीपों का समूह है। इसमें चार बड़े द्वीप हैं।
→ इनके नाम हैं-होंशू, क्यूशू, शिकोकू एवं होकाइदो। इनमें होंशू सबसे बड़ा है और जापान के केंद्र में है। जापान की 50 प्रतिशत से कुछ अधिक ज़मीन पहाड़ी है। जापान की केवल 17 प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती है।
→ जापान के पहाड़ों में अक्सर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। अतः जापान में भूकंप बहुत विनाश करते हैं। प्राचीन काल में जापानी सभ्यता चीनी सभ्यता से बहुत प्रभावित थी। जापान की अधिकाँश जनसंख्या जापानी है।
→ इसके अतिरिक्त यहाँ आयनू और कोरिया के कुछ लोग भी रहते हैं। जापान के लोगों का मुख्य भोजन चावल एवं मछली है। जापान की साशिमी अथवा सूशी नामक मछली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जापान में 1603 ई० से लेकर 1867 ई० तक तोकुगावा परिवार का शासन था। इस परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे।
→ शोगुन दैम्यो, प्रमुख शहरों एवं खदानों पर नियंत्रण रखते थे। 1853 ई० में संयुक्त राज्य अमरीका का नाविक कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जापान की बंदरगाह योकोहामा पहुँचने में सफल हुआ। 1854 ई० में उसने जापान। सरकार के साथ कानागावा नामक संधि की। इसे जापान का खलना कहा जाता है।
→ इस संधि के पश्चात जापान के दरवाजे पश्चिमी देशों के लिए खुल गए एवं जापान ने आधुनिकीकरण के रास्ते को अपनाया। जापान में सम्राट मत्सहितो ने 1868 ई० से 1912 ई० तक शासन किया। उसने मेज़ी की उपाधि धारण की थी। इसलिए इस काल को मेज़ी पुनर्स्थापना कहते हैं।
→ मेज़ी शासनकाल में जापान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए गए एवं उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई। जापान ने 1894-95 ई० में चीन को पराजित कर एवं 1904-05 ई० में रूस को पराजित कर विश्व को चकित कर दिया था।
→ उसने 1910 ई० में कोरिया जो उसके लिए सामरिक महत्त्व का था को भी अपने अधीन कर लिया। जापान में सैन्यवाद के कारण वहाँ सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने प्रमुख भूमिका निभाई। उसने अनेक सफलताएँ अर्जित की थीं।
→ 1945 ई० में अमरीका द्वारा हिरोशिमा एवं नागासाकी में गिराए गए दो एटम बमों के कारण उसे पराजय को स्वीकार करना पड़ा था। इस कारण जापान पर अमरीका का कब्जा हो गया था। यह कब्जा 1945 ई० से 1952 ई० तक रहा।
→ अमरीका के जापान से हटने के बाद उसने पुनः अपने गौरव को स्थापित किया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। वह 1956 ई० में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। उसने 1964 ई० में अपनी राजधानी तोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया।
→ दूसरी ओर चीन पूर्वी एशिया का एक अत्यंत प्राचीन एवं विशाल देश है। इस विशाल क्षेत्र में अनेक नदियाँ एवं पर्वत हैं। चीन की तीन नदियाँ-पीली नदी, यांग्त्सी नदी एवं पर्ल नदी ने चीनी सभ्यता के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
→ ये नदियाँ यातायात, सिंचाई एवं उर्वरता का प्रमुख साधन हैं। यहाँ लोहे, कोयले एवं ताँबे की प्रचुरता है। यहाँ अनेक जातीय समूह रहते हैं। हान यहाँ का प्रमुख जातीय समूह है। यहाँ की प्रमुख भाषा चीनी है। चीन का सबसे स्वादिष्ट भोजन डिम-सम है। चीनी चावल एवं गेहूँ का खूब प्रयोग करते हैं।
→ चीन शताब्दियों तक विदेशियों के लिए बंद रहा। 1839–42 ई० में ब्रिटेन ने चीन को प्रथम अफ़ीम युद्ध में पराजित कर उसके दरवाज़े पश्चिमी देशों के लिए खोल दिए। चीन आरंभ में जापान की तरह आधुनिकीकरण के रास्ते को सुगमता से अपनाने को तैयार नहीं था।
→ 1856-60 ई० में ब्रिटेन ने चीन को दूसरे अफ़ीम युद्ध में पुनः पराजित किया। इससे चीन की आंतरिक कमजोरी का भेद विश्व के अन्य देशों को पता चल गया। अतः विश्व के अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, फ्राँस, रूस, जापान आदि ने चीन के अनेक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया।
→ इससे चीन की अखंडता के लिए एक भारी ख़तरा उत्पन्न हो गया। चीन में बढ़ते हुए विदेशी प्रभाव एवं अन्य समस्याओं के चलते 1911 ई० में चीनी क्रांति का विस्फोट हो गया। इस क्राँति के कारण चीन में माँचू वंश का अंत हुआ।
→ इस क्राँति में डॉक्टर सन-यात-सेन ने उल्लेखनीय योगदान दिया। चीन में डॉक्टर सन-यात-सेन के नेतृत्व में 1912 ई० में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1925 ई० में डॉक्टर सन-यात-सेन की मृत्यु के पश्चात् चीन में पुनः संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस समय चीन में माओ-त्सेतुंग ने नेतृत्व किया।
→ उसने चीनी लोगों को एकत्र करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। उसके अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप चीन में 1949 ई० में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की सरकार अस्तित्व में आई। निस्संदेह यह चीन के इतिहास में एक नए युग का संदेश था।
→ माओ त्सेतुंग जिसे 1949 ई० में चीन का अध्यक्ष बनाया गया था ने 1976 ई० में अपनी मृत्यु तक उल्लेखनीय सुधार किए। परिणामस्वरूप वह चीनी समाज को एक नई दिशा देने में सफल रहा।
→ चियांग-काई-शेक ने 1949 ई० में माओ-त्सेतुंग से पराजित होने के पश्चात् ताइवान (फारमोसा) में चीनी गणतंत्र की स्थापना कर ली थी। वह स्वयं ताइवान का राष्ट्रपति बन गया। उसने बहुत सख्ती से शासन किया एवं मार्शल लॉ को लागू किया। उसने अपने सभी विरोधियों को कठोर दंड दिए।
→ उसने ताइवान की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के उद्देश्य से अनेक उल्लेखनीय कदम उठाए। वह इस उद्देश्य में काफी सीमा तक सफल रहा। 1975 ई० में चियांग-काई-शेक की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् चीन की राजनीति में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चीन एवं ताइवान का एकीकरण आज भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।
→ चीन एवं जापान में इतिहास लिखने की एक लंबी परंपरा रही है। इसका कारण यह था कि इसे शासकों के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए इन देशों के शासकों ने अभिलेखों की देख-रेख एवं राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की।
→ इन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान की गई। सिमा छियन (Sima Qian) को प्राचीन चीन का सबसे महान् इतिहासकार माना जाता है। आधुनिक इतिहासकारों में चीन के लिआंग छिचाओ (Liang Qichao) एवं जापान के कुमे कुनीताके (Kume Kunitake) के नाम उल्लेखनीय हैं।
→ इटली के यात्री मार्को पोलो (Marco Polo) एवं जैसूइट पादरी मैटियो रिक्की (Mateo Ricci) ने चीन के तथा लुई फ़रॉय ने जापान के इतिहास पर काफी प्रकाश डाला है।
→ चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोजफ नीडहम (Joseph Needham) ने एवं जापानी इतिहास एवं संस्कृति पर जॉर्ज सैन्सम (George Sansom) ने उल्लेखनीय कार्य किया है।
→ नाइतो कोनन (Naito Konan) एक प्रसिद्ध जापानी विद्वान् थे। उन्होंने चीनी इतिहास पर काफी कार्य किया। उन्होंने अपने कार्य में पश्चिमी इतिहास लेखन की नयी तकनीकों तथा पत्रकारिता के अपने अनुभवों का काफी प्रयोग किया है। उन्होंने 1907 ई० में क्योतो विश्वविद्यालय (Kyoto University) में प्राच्य अध्ययन का विभाग (Department of Oriental Studies) को स्थापित किया।
![]()
![]()
![]()
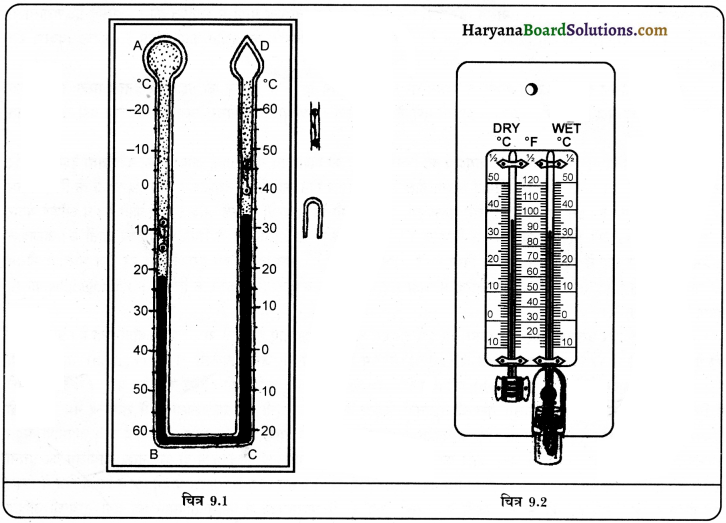
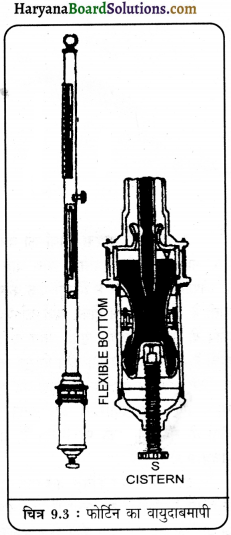

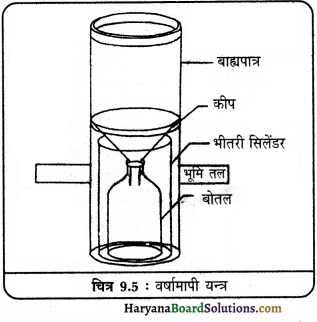
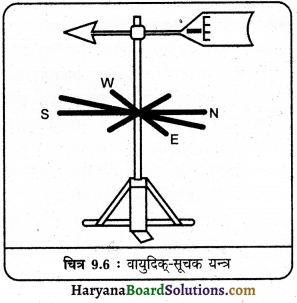
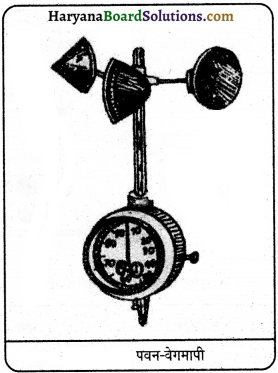
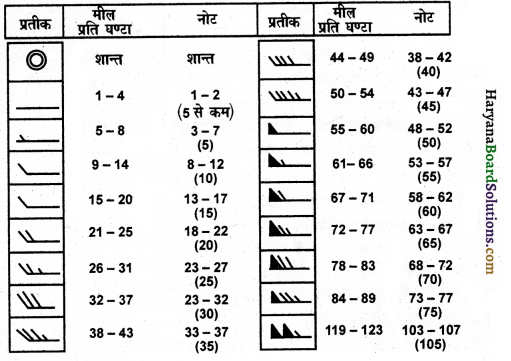
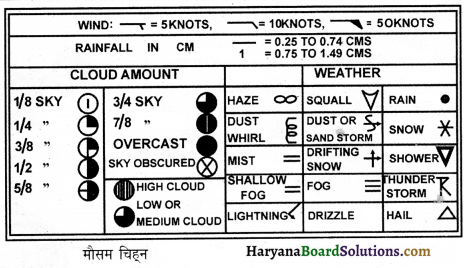
![]()
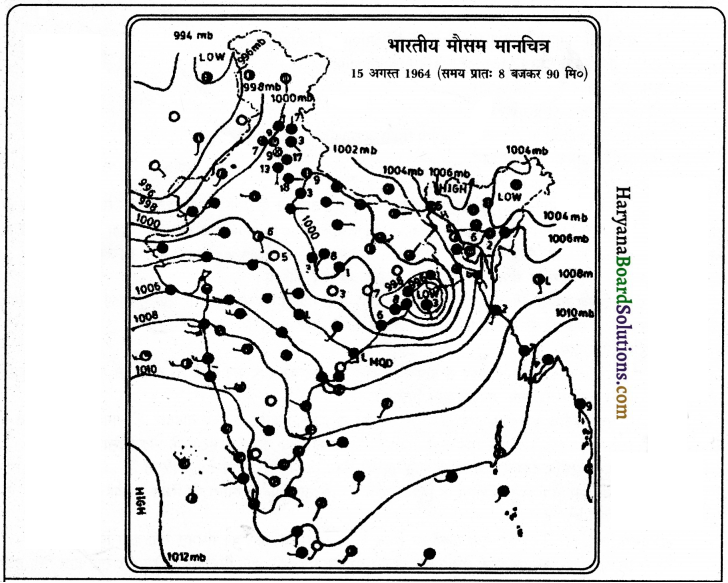
![]()