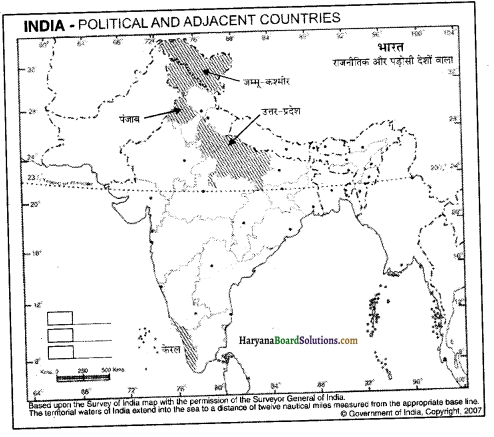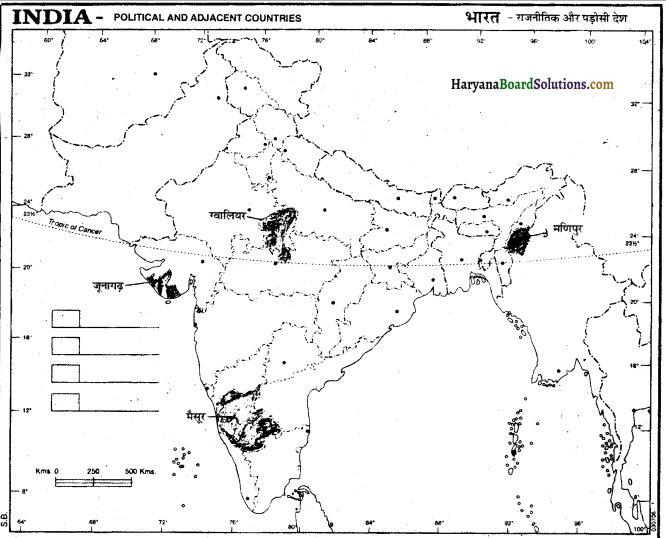Haryana State Board HBSE 12th Class Sociology Important Questions Chapter 3 सामाजिक संस्थाएँ : निरन्तरता एवं परिवर्तन Important Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Sociology Important Questions Chapter 3 सामाजिक संस्थाएँ : निरन्तरता एवं परिवर्तन
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1.
कौन-सा कथन असत्य है?
(A) वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है
(B) वर्ग में स्थिति अर्जित की जाती है
(C) वर्ग परिवर्तन असंभव नहीं है
(D) उपर्युक्त सभी कथन असत्य है।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी कथन असत्य है।
प्रश्न 2.
पूँजीपति और सर्वहारा वर्ग विभाजन किसकी देन है?
(A) मैक्स वैबर
(B) इमाइल दुर्थीम
(C) कार्ल मार्क्स
(D) स्वामी दयानंद।
उत्तर:
कार्ल मार्क्स।
प्रश्न 3.
निम्न में से कौन-सी विशेषता जनजाति की नहीं है?
(A) सामान्य नाम
(B) सामान्य क्षेत्र
(C) सामान्य बोली
(D) बहिर्विवाह।
उत्तर:
बहिर्विवाह।
प्रश्न 4.
कौन-सा कथन असत्य है?
(A) जाति में सामाजिक परिस्थिति अर्जित की जाती है
(B) वर्ग में सामाजिक स्थिति प्रदत्त होती है
(C) जनजाति एक अर्जित समूह है
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 5.
जाति को बनाए रखने में कौन-सी विशेषता सर्वाधिक अनिवार्य है?
(A) अंतर्विवाह वंशानुगत सदस्यता
(B) जातिगत व्यवसाय
(C) जातिगत विशेषधिकार
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 6.
किस वेद में पुरुष सूक्त में जाति की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है?
(A) ऋग्वेद
(B) यजुर्वेद
(C) अथर्ववेद
(D) सामवेद।
उत्तर:
ऋग्वेद।
प्रश्न 7.
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पास हुआ था?
(A) 1956
(B) 1954
(C) 1955
(D) 1957
उत्तर:
1955
प्रश्न 8.
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है?
(A) संथाल
(B) मुंडा
(C) टोडा
(D) हो।
उत्तर:
मुंडा।
प्रश्न 9.
किस संस्था ने भारतीय समाज को बुरी तरह विघटित किया है?
(A) जाति व्यवस्था
(B) वर्ग व्यवस्था
(C) संयुक्त परिवार
(D) दहेज प्रथा।
उत्तर:
जाति व्यवस्था।
प्रश्न 10.
इनमें से कौन-सा वर्ग का आधार है?
(A) पैसा
(B) पेशा
(C) जन्म
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 11.
जाति व्यवस्था का एक प्रकार्य बताइए।
(A) सामाजिक स्थिति को निश्चित करना
(B) अपनी योग्यताओं व क्षमताओं से प्राप्त करना
(C) सामाजिक संबंध स्वतंत्र रूप से रखना
(D) व्यवस्था को इच्छानुसार चुनना।
उत्तर:
सामाजिक स्थिति को निश्चित करना।
प्रश्न 12.
नातेदारी संगठन व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं, जो परस्पर-
(A) रक्त संबंधी होते हैं
(B) वैवाहिक संबंधी होते हैं
(C) रक्त और वैवाहिक संबंधी होते हैं
(D) रक्त या वैवाहिक संबंधी होते हैं
उत्तर:
रक्त संबंधी होते हैं।
प्रश्न 13.
सभी सगोत्रीय व्यक्ति रक्त संबंधी होने के कारण
(A) बहिर्विवाही होते हैं
(B) अंतर्विवाही होते हैं
(C) एकविवाही होते हैं
(D) उपर्युक्त सभी होते हैं।
उत्तर:
बहिर्विवाही होते हैं।
प्रश्न 14.
निम्न में से कौन-सा धर्म विधवा व तलाकशुदा स्त्री से विवाह को प्रोत्साहन देता है?
(A) ईसाई
(B) मुस्लिम
(C) हिंदू
(D) कोई नहीं।
उत्तर:
ईसाई।
प्रश्न 15.
निम्न में से कौन-सा कार्य परिवार से संबंधित नहीं है?
(A) वैध यौन संबंध
(B) समाज स्वीकृत संतोनत्पत्ति
(C) नातेदारी समूह निर्माण
(D) औपचारिक शिक्षा देना।
उत्तर:
वैध यौन संबंध।

प्रश्न 16.
हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है?
(A) धर्म, प्रजनन, रीत
(B) प्रजनन, धर्म, रीत
(C) रीत, प्रजनन, धर्म
(D) उपर्युक्त कोई नहीं।
उत्तर:
धर्म, प्रजनन, रीत।
प्रश्न 17.
अपने ही समूह में विवाह को क्या कहते हैं?
(A) समूह विवाह
(B) एक विवाह
(C) अंतर्विवाह
(D) बहिर्विवाह।
उत्तर:
अंतर्विवाह।
प्रश्न 18.
परिवार के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आ रहा है?
(A) नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के कारण
(B) स्त्रियों के घर से बाहर निकलने के कारण
(C) स्त्रियों की शिक्षा बढ़ने के कारण
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 19.
बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ शुरू होता है?
(A) परिवार में
(B) स्कूल में
(C) पड़ोस में
(D) खेल समूह में।
उत्तर:
परिवार में।
प्रश्न 20.
हिंदू विवाह को क्या समझा जाता है?
(A) समझौता
(B) धार्मिक संस्कार
(C) मित्रता
(D) सहयोग की प्रक्रिया।
उत्तर:
धार्मिक संस्कार।
प्रश्न 21.
हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ?
(A) 1950
(B) 1952
(C) 1955
(D) 1953
उत्तर:
1955
प्रश्न 22.
एक व्यक्ति के जीवन में परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण समूह है क्योंकि-
(A) सदस्यों का एक-दूसरे के प्रति निःस्वार्थ समर्पण होता है।
(B) सदस्य रक्त, विवाह तथा दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित होते हैं।
(C) परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक तथा सामाजिक समर्थन प्रदान करता है।
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
उपरोक्त सभी।
प्रश्न 23.
वह नातेदारी व्यवहार जिसमें मामा महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
(A) साहप्रसीवता
(B) परिहार
(C) मातुलेय
(D) परिहास संबंध।
उत्तर:
मातुलेय।
प्रश्न 24.
दहेज निषेध कानून प्रथम बार कब लागू हुआ?
(A) 1960
(B) 1959
(C) 1958
(D) 1961
उत्तर:
1961
प्रश्न 25.
परिवार का महत्त्वपूर्ण प्रकार्य है
(A) भौतिक सुरक्षा प्रदान करना
(B) आर्थिक समर्थन प्रदान करना
(C) सामाजिक मानदंडों के अनुसार बच्चे का समाजीकरण करना।
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
उपरोक्त सभी।
प्रश्न 26.
एक गोत्र ऐसा नातेदारी (स्वजन) समूह होता है-
(A) जिसके सदस्य अपने आपको किसी ज्ञात पूर्वज के वंशज मानते हैं।
(B) जिसके सदस्यों का विश्वास होता है कि वे एक ही मिथकीय पूर्वज के वंशज हैं।
(C) जिसके उदाहरण हैं माता-पिता तथा बच्चे
(D) उपरोक्त कोई नहीं।
उत्तर:
जिसके सदस्य अपने आपको किसी ज्ञात पूर्वज के वंशज मानते हैं।
प्रश्न 27.
संयुक्त परिवार में-
(A) परिवार में मुखिया के आदेशों का पालन करना होता है।
(B) सदस्यों की प्रस्थिति उनकी आय या व्यावसायिक उपलब्धि पर आधारित नहीं होती।
(C) प्रत्येक सदस्य, दूसरे सदस्य के सुख-दुःख को बाँटता है।
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
उपरोक्त सभी।
प्रश्न 28.
नातेदारी व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि-
(A) यह उसे स्थिति एवं पहचान प्रदान करती है
(B) यह मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है
(C) यह उसके व्यवहार तथा भूमिका को परिभाषित सुनिश्चित करती है
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
उपरोक्त सभी।
प्रश्न 29.
भारत में लिंग निर्धारण परीक्षणों को एक अधिनियम द्वारा कब निषिद्ध किया गया?
(A) 1990
(B) 1993
(C) 1994
(D) 1991
उत्तर:
1990
प्रश्न 30.
निम्न में से कौन-सा मानव समाज की मूल संस्थाओं में से नहीं है?
(A) नातेदारी
(B) आर्थिक
(C) राजनीति
(D) खेलकूद।
उत्तर:
खेलकूद।
प्रश्न 31.
निम्नलिखित में से कौन केंद्रक (एकांकी) परिवार का सदस्य नहीं है?
(A) माता
(B) पिता
(C) नाना
(D) भाई।
उत्तर:
नाना।
प्रश्न 32.
जनजाति निम्नोकत में से कौन-सा समूह है?
(A) भौगोलिक
(B) भाषाई
(C) संजातीय
(D) इनमें से सभी।
उत्तर:
इनमें से सभी।
प्रश्न 33.
पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे कैसे परिवार का निर्माण करते हैं?
(A) केंद्रक परिवार
(B) नगरीय परिवार
(C) संयुक्त परिवार
(D) ग्रामीण परिवार।
उत्तर:
केंद्रक परिवार।
प्रश्न 34.
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया?
(A) 1852 में
(B) 1856 में
(C) 1860 में
(D) 1864 में
उत्तर:
1856 में।
प्रश्न 35.
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है?
(A) बड़ा आकार
(B) छोटा आकार
(C) सामान्य रसोई
(D) मुखिया की भूमिका।
उत्तर:
छोटा आकार।
प्रश्न 36.
निम्न में से वर्ग एक क्या है?
(A) समाज
(B) समिति
(C) खुली व्यवस्था
(D) बंद व्यवस्था।
उत्तर:
खुली व्यवस्था।
प्रश्न 37.
मातृ-वंशीय परिवार प्रथा प्रचलित है :
(A) खासी परिवारों में
(B) भील
(C) संथाल
(D) ओरांव।
उत्तर:
खासी परिवारों में।
प्रश्न 38.
जब कोई वंश पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो कहलाता है:
(A) वर्ण
(B) वर्ग
(C) समूह
(D) जाति।
उत्तर:
जाति।
प्रश्न 39.
निम्न में से कम-से-कम किस आयु का बच्चा सामाजिक संबंधों के बारे में जानता है?
(A) 6 वर्ष का
(B) 10 वर्ष का
(C) 18 वर्ष का
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
……………… व्यवस्था ने हमारे समाज को बाँट दिया है।
उत्तर:
जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को बाँट दिया है।
प्रश्न 2.
शब्द Caste किस भाषा के शब्द से निकला है?
उत्तर:
शब्द Caste पुर्तगाली भाषा के शब्द से निकला है।
प्रश्न 3.
जाति किस प्रकार का वर्ग है?
उत्तर:
बंद वर्ग।
प्रश्न 4.
जाति प्रथा में किसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी?
उत्तर:
जाति प्रथा में ब्राह्मणों को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी।
प्रश्न 5.
अंतर्विवाह का क्या अर्थ है?
उत्तर:
जब व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करवाना पड़ता है तो उसे अंतर्विवाह कहते हैं।
प्रश्न 6.
जाति में व्यक्ति का पेशा किस प्रकार का होता है?
उत्तर:
जाति में व्यक्ति का पेशा जन्म पर आधारित होता है अर्थात् व्यक्ति को अपने परिवार का परंपरागत पेशा अपनाना पड़ता है।
प्रश्न 7.
जाति में आपसी संबंध किस पर आधारित होते हैं?
उत्तर:
जाति में आपसी संबंध उच्चता तथा निम्नता पर आधारित होते हैं।
प्रश्न 8.
अगर जाति आवृत्त है तो वर्ग ………………. है।
उत्तर:
अगर जाति आवृत्त है तो वर्ग अनावृत्त है।
प्रश्न 9.
आवृत्त जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है?
उत्तर:
जो वर्ग बदला नहीं जा सकता उसे आवृत्त जाति व्यवस्था कहते हैं।

प्रश्न 10.
कच्चा भोजन तथा पक्का भोजन बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है?
उत्तर:
कच्चा भोजन बनाने के लिए पानी तथा पक्का भोजन बनाने के लिए घी का प्रयोग होता है।
प्रश्न 11.
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पास हुए थे?
उत्तर:
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में पास हुआ था।
प्रश्न 12.
हिंदू विवाह अधिनियम …………….. में पास हुआ था।
उत्तर:
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में पास हुआ था।
प्रश्न 13.
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में किस बात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था?
उत्तर:
इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्य कहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
प्रश्न 14.
सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है?
उत्तर:
समाज को उच्च तथा निम्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं।
प्रश्न 15.
भारत में लगभग कितनी जातियाँ पाई जाती हैं?
उत्तर:
भारत में लगभग 3000 जातियाँ पाई जाती हैं।
प्रश्न 16.
जनजातियों के व्यवसाय किस पर आधारित होते हैं?
उत्तर:
जनजातियों के व्यवसाय जंगलों पर आधारित होते हैं।
प्रश्न 17.
जाति किस प्रकार के विवाह की अनुमति देती है?
उत्तर:
जाति अंतर्विवाह की अनुमति देती है।
प्रश्न 18.
जनजातीय समाज का आकार कैसा होता है?
उत्तर:
जनजातीय समाज छोटे आकार के होते हैं।
प्रश्न 19.
जो लोग आम जीवन से दूर जंगलों पहाड़ों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
उत्तर:
जो लोग आम जीवन से दूर जंगलों पहाड़ों में रहते हैं उन्हें जनजाति अथवा कबीला कहते हैं।
प्रश्न 20.
प्राचीन भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था?
उत्तर:
प्राचीन भारतीय समाज चार भागों में विभाजित था।
प्रश्न 21.
जाति व्यवस्था का क्या लाभ था?
उत्तर:
इसने हिंदू समाज का बचाव किया, समाज को स्थिरता प्रदान की तथा लोगों को एक निश्चित व्यवसाय प्रदान किया था।
प्रश्न 22.
परंपरागत तथा आदिम समाजों में वर्ग स्थिति में महत्त्वपूर्ण कारक कौन-सा था?
उत्तर:
परंपरागत तथा आदिम समाजों में वर्ग स्थिति में महत्त्वपूर्ण कारक धर्म था।
प्रश्न 23.
जनजातियों में किस चीज़ का अधिक महत्त्व होता है?
उत्तर:
जनजातियों में टोटम का अधिक महत्त्व होता है।
प्रश्न 24.
मजूमदार ने जनजातियों को कितने वर्गों में बांटा है?
उत्तर:
मजूमदार ने जनजातियों को तीन वर्गों में बांटा है।
प्रश्न 25.
नीलगिरी पहाड़ियों में कौन-सी जनजाति रहती है?
उत्तर:
नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है।
प्रश्न 26.
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है?
उत्तर:
मुंडा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है।
प्रश्न 27.
खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है?
उत्तर:
असम में।
प्रश्न 28.
जनजातीय समाज आकार में कैसा होता है?
उत्तर:
जनजातीय समाज आकार में छोटा होता है।
प्रश्न 29.
जनजातीय जीवन किस पर आधारित होती है?
उत्तर:
जनजातीय जीवन बंधुता पर आधारित है।
प्रश्न 30.
भारत में आजकल कितनी जनजातियाँ पायी जाती हैं?
उत्तर:
आजकल भारत में 425 के लगभग जनजातियाँ पायी जाती हैं।
प्रश्न 31.
जनजातीय भाषाएं किस से संबंधित हैं?
उत्तर:
जनजातियों की भाषाएं आस्ट्रिक, द्रविड़ियन तथा तिब्बती चीनी से संबंधित हैं।
प्रश्न 32.
सजातीय विवाह क्या होता है?
उत्तर:
अपनी ही जाति, उपजाति या समूह में विवाह करना सजातीय विवाह होता है।
प्रश्न 33.
घुमंतू जनजाति क्या होती है?
उत्तर:
यह शिकारी तथा भोजन इकट्ठा करने वाली जनजाति होती है जो कि घने जंगलों में घूमती है। यह अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए घूमते रहते हैं। कुछ नागा जनजातियाँ इसी श्रेणी में आती हैं।
प्रश्न 34.
झूम खेती कौन करता है?
उत्तर:
झूम खेती जनजातीय समूह करते हैं।
प्रश्न 35.
झारखंड में कौन-सी जनजातियाँ पायी जाती हैं?
उत्तर:
मुंडा, उराव, संथाल इत्यादि जनजातियाँ पायी जाती हैं।
प्रश्न 36.
अंग्रेज़ों ने जनजातियों को किस आधार पर अलग किया?
उत्तर:
अंग्रेजों ने जनजातियों को धार्मिक तथा स्थानीय आधारों पर अलग किया।
प्रश्न 37.
नीलगिरी पहाड़ियों में कौन-सी जनजाति रहती है?
उत्तर:
टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है।
प्रश्न 38.
सबसे अधिक जनजातियाँ किस राज्य में पायी जाती हैं?
उत्तर:
सबसे अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पायी जाती हैं।
प्रश्न 39.
एक विवाह का क्या अर्थ है?
उत्तर:
जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहते हैं।
प्रश्न 40.
बहुविवाह के कितने प्रकार हैं?
उत्तर:
बहुविवाह के तीन प्रकार हैं।
प्रश्न 41.
विविवाह में एक पुरुष की कितनी पत्नियां होती हैं?
उत्तर:
द्विविवाह में एक पुरुष की दो पत्नियां होती हैं।
प्रश्न 42.
बहुपति विवाह में एक स्त्री के कितने पति हो सकते हैं?
उत्तर:
बहुपति विवाह में एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं।
प्रश्न 43.
पितृ सत्तात्मक परिवार में …………………. की शक्ति अधिक होती है।
उत्तर:
पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता की शक्ति अधिक होती है।
प्रश्न 44.
मातृ सत्तात्मक परिवार में ………………. की सत्ता चलती है।
उत्तर:
मात सत्तात्मक परिवार में माता की सत्ता चलती है।
प्रश्न 45.
किस परिवार में वंश का नाम पिता के नाम से चलता है?
उत्तर:
पितृवंशी परिवार में वंश का नाम पिता के नाम से चलता है।
प्रश्न 46.
रक्त संबंधी परिवार में कौन-से संबंध पाए जाते हैं?
उत्तर:
रक्त संबंधी परिवार में रक्त संबंध पाए जाते हैं।
प्रश्न 47.
आगमन परिवार का अर्थ बताएं।
उत्तर:
जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता तथा बड़ा होता है उसे आगमन परिवार कहते हैं।
प्रश्न 48.
कौन-से परिवार को संतान पैदा करने वाला परिवार कहा जाता है?
उत्तर:
जन्म परिवार को।
प्रश्न 49.
नातेदारी कितने प्रकारों में बांटी जा सकती है?
उत्तर:
नातेदारी तीन प्रकारों में बांटी जा सकती है।
प्रश्न 50.
रक्त संबंधी किस नातेदारी के भाग होते हैं?
उत्तर:
रक्त संबंधी सगोत्र नातेदारी के भाग होते हैं।

प्रश्न 51.
सिबलिंग (Sibling) का अर्थ बताएं।
उत्तर:
सगे भाई बहन को सिबलिंग कहा जाता है।
प्रश्न 52.
हाफ सिबलिंग (Half Sibling) का अर्थ बताएं।
उत्तर:
सौतेले भाई-बहन को हाफ सिबलिंग कहा जाता है।
प्रश्न 53.
एक रेखीय संबंधी कौन-से होते हैं?
उत्तर:
वंशक्रम की सीधी रेखा के साथ संबंधित रिश्तेदारों को एक रेखीय संबंधी कहते हैं।
प्रश्न 54.
वंश समूह का अर्थ बताएं।
उत्तर:
माता अथवा पिता के रक्त संबंधियों को मिलाकर वंश समूह बनता है।
प्रश्न 55.
गोत्र ………………… का विस्तृत रूप है।
उत्तर:
गोत्र वंश समूह का विस्तृत रूप है।
प्रश्न 56.
सदस्यों के आधार पर परिवार के कितने तथा कौन-से प्रकार होते हैं?
उत्तर:
सदस्यों के आधार पर परिवार के तीन प्रकार केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार होते हैं।
प्रश्न 57.
विवाह के आधार पर परिवार के कितने तथा कौन-से प्रकार होते हैं?
उत्तर:
विवाह के आधार पर परिवार के दो प्रकार-एक विवाही परिवार तथ होते हैं।
प्रश्न 58.
वंश के आधार पर कितने प्रकार के परिवार होते हैं?
उत्तर:
चार प्रकार के परिवार।
प्रश्न 59.
अंतर्विवाह क्या है?
उत्तर:
जब व्यक्ति केवल अपनी ही जाति में विवाह करवा सकता हो उसे अंतर्विवाह कहा जाता है।
प्रश्न 60.
बर्हिविवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर:
जब व्यक्ति को अपनी गोत्र के बाहर परंतु अपनी जाति के अंदर विवाह करवाना पड़े तो उसे बर्हिविवाह कहते हैं।
प्रश्न 61.
केंद्रीय परिवार का अर्थ बताएं।
अथवा
मूल परिवार क्या है?
उत्तर:
वह परिवार जिसमें पति पत्नी तथा उनके बिनब्याहे बच्चे रहते हों उसे केंद्रीय परिवार अथवा मूल परिवार कहा जाता है।
प्रश्न 62.
मुस्लिम तलाक कानून कंब पास हुआ था?
उत्तर:
मुस्लिम तलाक कानून, 1954 में पास हुआ था।
प्रश्न 63.
ईसाइयों का तलाक कानून …………………. में पास हुआ था।
उत्तर:
ईसाइयों का तलाक कानून 1869 में पास हुआ था।
प्रश्न 64.
हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पास हुआ था?
उत्तर:
सन् 1856 में।
प्रश्न 65.
किस समुदाय में मेहर की प्रथा प्रचलित है?
उत्तर:
मुस्लिम समुदाय में।
प्रश्न 66.
विशेष विवाह अधिनियम कब पास हुआ था?
उत्तर:
विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पास हुआ था।
प्रश्न 67.
संयुक्त परिवार के विघटित होने का क्या कारण है?
उत्तर:
पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, यातायात के साधनों का विकास इत्यादि के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं।
प्रश्न 68.
संयुक्त परिवार में संपत्ति पर किसका अधिकार होता है?
उत्तर:
संयुक्त परिवार में संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार होता है।
प्रश्न 69.
टेलर के अनुसार परिवार की प्रकृति क्या थी?
उत्तर:
टेलर के अनुसार आदिम परिवार मातृ प्रधान थे।
प्रश्न 70.
केंद्रीय परिवार की एक विशेषता बताएं।
उत्तर:
केंद्रीय परिवार में पति पत्नी तथा उनके बिन-ब्याहे बच्चे रहते हैं तथा परिवार के सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
प्रश्न 71.
परिवार के आरंभिक कार्य क्या हैं?
उत्तर:
परिवार के आरंभिक कार्य हैं लैंगिक संबंधों की पूर्ति, बच्चे पैदा करना तथा बच्चों का पालन-पोषण करना।
प्रश्न 72.
गारो जनजाति में वंश परंपरा किस प्रकार की होती है?
उत्तर:
गारो जनजाति में वंश परंपरा पितृस्थानीय प्रकार की होती है।
प्रश्न 73.
माता-पिता, भाई-बहन, माँ-बेटा, पिता-पुत्री का संबंध कैसा होता है?
उत्तर:
इन सब का संबंध रक्त का होता है।
प्रश्न 74.
मातृवंशी परिवार में संपत्ति किसको मिलती है?
उत्तर:
मातृवंशी परिवार में संपत्ति पुत्री को प्राप्त होती है।
प्रश्न 75.
पति-पत्नी, जमाई-ससुर, जीजा-साला इत्यादि किस प्रकार के संबंध हैं?
उत्तर:
विवाह संबंधी हैं।
प्रश्न 76.
नातेदारी की …………………. श्रेणियां हैं।
उत्तर:
नातेदारी की तीन श्रेणियां हैं।
प्रश्न 77.
नातेदारी की प्राथमिक श्रेणी में कितने प्रकार के संबंध होते हैं?
उत्तर:
नातेदारी की प्राथमिक श्रेणी में 8 प्रकार के संबंध होते हैं।
प्रश्न 78.
माता-पिता व बच्चों का संबंध नातेदारी की कौन-सी श्रेणी में आता है?
उत्तर:
प्राथमिक श्रेणी में।
प्रश्न 79.
जिसके सदस्य अपने आपको किसी जात पूर्वज के वंशज मानते हैं ऐसा समूह ……………. कहलाता
उत्तर:
गोत्र।
प्रश्न 80.
किसी एक ऐसी मुख्य जनजाति का नाम बताइये जिसकी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की हो।
उत्तर:
इरूला, कुर्ग।
प्रश्न 81.
जनजातीय लोग कौन-से इलाके में अधिक रहते हैं?
उत्तर:
जनजातीय लोग मुख्यता पहाड़ियों, वनों, ग्रामीण मैदान और नगरीय औद्योगिक इलाकों में रहते हैं।
प्रश्न 82.
एक ऐसा परिवार जिसमें नवविवाहिता दंपत्ति वर के मामा के निवास स्थान पर रहते हैं, कहलाता है …………….।
उत्तर:
मातृवंशीय परिवार।
प्रश्न 83.
वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है ……………… कहलाता है।
उत्तर:
जनन परिवार।
प्रश्न 84.
एक व्यक्ति का जीजा किस श्रेणी की नातेदारी का होगा?
उत्तर:
द्वितीय श्रेणी की नातेदारी।
प्रश्न 85.
जनजाति में बंधुआ मज़दूरी का कारण क्या है?
उत्तर:
इसका कारण उनके ऊपर चढ़ा कर्ज है। वह कर्ज चुका नहीं पाते हैं जिस कारण उन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है।
प्रश्न 86.
जाति का अर्थ बताएँ।
अथवा
जाति क्या है?
अथवा
जाति का अर्थ लिखें।
उत्तर:
हिंदू सामाजिक प्रणाली में एक उलझी हुई एवं दिलचस्प संस्था है जिसका नाम ‘जाति व्यवस्था’ है। यह शब्द पुर्तगाली शब्द ‘Casta’ से लिया गया है जिसका अर्थ है ‘जन्म’। इस प्रकार यह एक अंत-वैवाहिक जिसकी सदस्यता जन्म के ऊपर आधारित है। इसमें कार्य (धंधा) पैतृक एवं परंपरागत होता है।
प्रश्न 87.
जाति व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं बतायें।
अथवा
जाति की एक विशेषता लिखिए।
अथवा
जाति की कोई दो सामान्य विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
- जाति की सदस्यता जन्म के आधार द्वारा होती है।
- जाति में सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध होते थे।
- जाति में खाने-पीने के बारे में प्रतिबंध होते थे।
प्रश्न 88.
पुरातन भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था?
उत्तर:
चार भागों में-
- ब्राह्मण-जो शिक्षा देने का काम किया करते थे।
- क्षत्रिय-जो देश की रक्षा करते थे तथा राज्य चलाते थे।
- वैश्य-जो व्यापार या खेती करते थे।
- चौथा वर्ण-जो अन्य तीन वर्गों की सेवा किया करते थे।
प्रश्न 89.
संस्कृति में हस्तांतरण में जाति की क्या भूमिका है?
उत्तर:
प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति, रहन-सहन, खाने-पीने, काम करने के ढंग तथा कुछ खास गुर होते हैं। व्यक्ति जब बचपन से ही इन सब को देखता है तो धीरे-धीरे वह इन सब को सीख जाता है। इस तरह जाति संस्कृति के हस्तांतरण में विशेष भूमिका निभाती है।
प्रश्न 90.
जाति प्रथा दैवी शक्ति से भी मज़बूत कैसे हैं?
उत्तर:
सदियों से जाति प्रथा हमारे समाज के राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन का आधार थी। हर किसी को जाति प्रथा के नियम मानने ही पड़ते थे। व्यक्ति भगवान का आदेश तो ठुकरा सकता था, परंतु अपनी जाति के आदेश उसे मानने ही पड़ते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा देवी शक्ति से भी ज्यादा मज़बूत थी।
प्रश्न 91.
जाति व्यवस्था के कोई तीन प्रभाव बताओ।
उत्तर:
- जाति व्यवस्था से समाज में श्रम विभाजन होता था।
- जाति व्यवस्था से सामाजिक संगठन बना रहता था।
- जाति व्यवस्था से राजनीतिक स्थिरता बनी रहती थी।
- जाति व्यवस्था बेरोज़गारी को कम करती थी।
प्रश्न 92.
जाति व्यवस्था के कोई तीन लाभ बताओ।
उत्तर:
- जाति से व्यवसाय निश्चित हो जाता था।
- जाति व्यवस्था समाज को स्थिरता प्रदान करती थी।
- जाति व्यवस्था में विवाह करने में परेशानी नहीं होती थी।

प्रश्न 93.
जाति की दो परिभाषाएं दीजिए।
अथवा
जाति की परिभाषा दीजिए।
उत्तर:
- होकार्ट के अनुसार, “जाति तो केवल कुछ ऐसे परिवारों का इकठ्ठ होती है जिन्हें जन्म से ही धार्मिक संस्कारों के आधार पर अलग-अलग प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं।”
- कूले के अनुसार, “जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है, तो हम उसे जाति कहते हैं।”
प्रश्न 94.
जाति व्यवस्था के तीन दोष अथवा हानियां बताएं।
उत्तर:
- जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि इस व्यवस्था में निम्न जातियों का शोषण होता था।
- जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में अस्पृश्यता की प्रथा को जन्म दिया था।
- जाति व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है।
प्रश्न 95.
जाति व्यवस्था में कौन-से परिवर्तन आ रहे हैं?
अथवा
जाति व्यवस्था में किसी एक परिवर्तन को बताइए।
अथवा
जाति प्रथा में कोई दो परिवर्तन बताएं।
उत्तर:
आधुनिक समय में शिक्षा के बढ़ने से, औद्योगिकीकरण के आने से, संचार के साधनों, नगरीकरण इत्यादि के कारण बहुत से परिवर्तन जाति व्यवस्था में आए हैं। जाति व्यवस्था के प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह बढ़ रहे हैं, निम्न जातियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, प्रत्येक प्रकार का भेदभाव खत्म हो रहा है तथा व्यवसाय की विशेषता खत्म हो गई है।
प्रश्न 96.
अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं?
अथवा
जनजाति का अर्थ लिखें।
अथवा
जनजाति से आप क्या समझते हैं?
अथवा
अनुसूचित जनजाति के बारे में बताइए।
अथवा
जनजाति क्या होती है?
उत्तर:
जनजाति एक ऐसा समुदाय होता है जो हमारी सभ्यता से दूर पहाड़ों, वनों तथा जंगलों में रहता है। इन समुदायों की अपनी ही अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग धर्म तथा खाने-पीने और रहने के अलग ही ढंग होते हैं। ये न तो किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तथा न ही किसी को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने की आज्ञा देते हैं। जिस जनजाति का नाम संविधान में दर्ज है उसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं।
प्रश्न 97.
जनजाति की एक परिभाषा दीजिए।
अथवा
जनजाति को परिभाषित करें।
अथवा
जनजाति क्या है?
उत्तर:
भारत में इंपीरियल गजेटियर के अनुसार, “जनजाति परिवारों का ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, एक सामान्य प्रदेश में रहता है अथवा रहने का दावा करता है और प्रायः अंतर्विवाह करने वाला नहीं होता, चाहे शुरू में उसमें अंतर्विवाह करने की रीति रही हो।”
प्रश्न 98.
जनजाति की दो विशेषताएं बताएं।
उत्तर:
- कबीला बहुत-से परिवारों का समूह होता है जिसमें साझा उत्पादन होता है तथा उस उत्पादन से वह अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं।
- कबीलों के लोग एक साझे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण यह शेष समाज से अलग होते तथा रहते हैं।
प्रश्न 99.
टोटम का अर्थ बताएं।
उत्तर:
जनजातियों में टोटम के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। यह टोटम एक काल्पनिक पूर्वज, पेड़, फल, पशु, पत्थर इत्यादि कुछ भी हो सकता है। जनजाति के सदस्य टोटम को पवित्र मानते हैं। उसे वह खाते या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फल व पौधे के रूप में टोटम में दैवी शक्ति है वे ऐसा विश्वास करते हैं।
प्रश्न 100.
परिवार का क्या अर्थ है?
उत्तर:
परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा जो इतना छोटा व स्थायी है कि उससे बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन-पोषण हो सके। इस प्रकार परिवार पति-पत्नी व उनके बच्चों से मिलकर बनता है। पति-पत्नी के बीच किसी न किसी प्रकार के स्थायी संबंध परिवार की मुख्य विशेषता है।
प्रश्न 101.
संयुक्त परिवार को परिभाषित करें।
अथवा
ग्रामीण भारतीय परिवार की परिभाषा दीजिए।
अथवा
संयुक्त परिवार क्या है?
अथवा
संयुक्त परिवार का अर्थ बताएँ।
अथवा
संयुक्त परिवार किसे कहते हैं?
उत्तर:
ग्रामीण भारतीय परिवार मुख्यतः संयुक्त परिवार होते हैं। इसलिए इरावती कार्वे के अनुसार, “एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतया एक मकान में रहते हैं, जो एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के भागी होते हैं, जो सामान्य रूप से पूजा में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार से एक-दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं।”
प्रश्न 102.
परिवार की दो विशेषताएं बताएं।
उत्तर:
- परिवार पति-पत्नी तथा उनके बच्चों से मिलकर बनता है। इस प्रकार पति-पत्नी के बीच किसी न किसी प्रकार के स्थायी संबंध परिवार की मुख्य विशेषता है। प्रत्येक संस्कृति में यह संबंध स्थायी होते हैं।
- वैवाहिक संबंध के आधार पर परिवार का जन्म होता है। यह संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इन संबंधों के आधार पर पति-पत्नी में लिंग संबंध से संतान उत्पन्न होती है जिन्हें मान्यता प्राप्त होती है।
प्रश्न 103.
परिवार के दो आर्थिक कार्य बताएं।
अथवा
परिवार का एक प्रकार्य लिखें।
उत्तर:
- परिवार में व्यक्ति की संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। परिवार अपने सदस्यों में समान रूप से सम्पत्ति विभाजित करता है।
- प्रत्येक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। परिवार की हरेक प्रकार की आवश्यकता, खाने-पीने, रहने तथा पहनने की व्यवस्था परिवार द्वारा ही पूर्ण की जाती है।
प्रश्न 104.
परिवार के दो सामाजिक कार्य बताएं।
उत्तर:
- बच्चों का समाजीकरण करने में परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। परिवार में रहकर ही बच्चा अच्छी आदतें सीखता है तथा समाज का एक अच्छा नागरिक बनता है।
- यदि हम सामाजिक नियंत्रण के साधनों की तरफ देखें तो परिवार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि परिवार ही व्यक्ति को नियंत्रण में रहना सिखाता है।
प्रश्न 105.
संयुक्त परिवार को बनाकर रखने वाले दो कारक बताएं।
उत्तर:
- धर्म ने संयुक्त परिवार को बनाकर रखा है। धर्म भारतीय सामाजिक संगठन का मूल आधार है। अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य संयुक्त रूप से करने होते हैं जिस कारण संयुक्त परिवार बना रह पाया है।
- हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जहाँ पर कृषि करने के लिए बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस कारण भी संयुक्त परिवार बने रहे।
प्रश्न 106.
परिवार के मनोरंजनात्मक कार्य के बारे में बताएँ।
उत्तर:
परिवार अपने सदस्यों को मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है। रात के समय परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं और अपने विचारों व मुश्किलों को एक-दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। परिवार के वृद्ध सदस्य बच्चों को दिलचस्प कथा-कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करते हैं। त्योहारों के समय या किसी अन्य जश्न (खुशी) के समय परिवार के सारे सदस्य नाचते व गाते हैं।
प्रश्न 107.
केंद्रीय परिवार क्या है?
अथवा
एकाकी (मूल) परिवार किसे कहते हैं?
अथवा
केंद्रक परिवार को पारिभाषित करें।
उत्तर:
केंद्रीय परिवार वह परिवार है जिसमें पति-पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। विवाह के बाद बच्चे अपना अलग घर कायम कर लेते हैं। यह सबसे छोटे परिवार होते हैं। यह परिवार अधिक प्रगतिशील होते हैं व उनके निर्णय तर्क के आधार पर होते हैं। इसमें पति-पत्नी को बराबर का दर्जा हासिल होता है।
प्रश्न 108.
केंद्रीय परिवार की विशेषताएं बताएं।
उत्तर:
- केंद्रीय परिवार या इकाई परिवार आकार में छोटा होता है।
- केंद्रीय परिवार में संबंध सीमित होते हैं।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को महत्ता मिलती है।
प्रश्न 109.
केंद्रीय परिवार के तीन गुण बताएं।
उत्तर:
- केंद्रीय परिवारों में स्त्रियों की स्थिति ऊँची होती है।
- इसमें रहन-सहन का दर्जा उच्च वर्ग का होता है।
- व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है।
प्रश्न 110.
केंद्रीय परिवार के अवगुण बताएं।
उत्तर:
- यदि माता या पिता में से कोई बीमार पड़ जाए तो घर के कामों में रुकावट आ जाती है।
- इसमें बेरोज़गार व्यक्ति का गुजारा मुश्किल से होता है।
- पति की मौत के पश्चात यदि स्त्री अशिक्षित हो तो परिवार की पालना कठिन हो जाती है।
प्रश्न 111.
विस्तृत परिवार का क्या अर्थ है?
उत्तर:
इस प्रकार के परिवार संयुक्त परिवार से ही बनते हैं। जब संयुक्त परिवार आगे बढ़ जाते हैं तो वह विस्तृत परिवार कहलाते हैं। इसमें माता-पिता, उनके भाई-बहन, बेटे-बेटियां व पोते-पोतियां आदि इकट्ठे रहते हैं। बच्चों के दादा-दादी भी इसमें रहते हैं। इस प्रकार इसमें कम से कम तीन पीढ़ियां रहती हैं।
प्रश्न 112.
संयुक्त परिवार का अर्थ बताएं।
उत्तर:
संयुक्त परिवार एक मुखिया की ओर से शासित अनेकों पीढ़ियों के रक्त संबंधियों का एक ऐसा समूह है जिनका निवास, चूल्हा व संपत्ति संयुक्त होते हैं। वह सब कर्तव्यों व बंधनों में बंधे रहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं-
- साँझा चूल्हा
- साँझा निवास
- साँझी संपत्ति
- मुखिया का शासन
- बड़ा आकार।
आजकल इस प्रकार के परिवारों की अपेक्षा केंद्रीय परविार चलन में आ गए हैं।
प्रश्न 113.
पितृ-मुखी परिवार क्या है?
अथवा
पितृवंशी परिवार क्या है?
अथवा
पितृसत्तात्मक परिवार क्या है?
उत्तर:
जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रकार के परिवारों की सत्ता या शक्ति पूरी तरह से पिता के हाथ में होती है। परिवार के संपूर्ण कार्य पिता के हाथ में होते हैं। वह ही परिवार का कर्ता होता है। परिवार के सभी छोटे या बड़े कार्यों में पिता का ही कहना माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों पर पिता का ही नियंत्रण होता है। इस तरह का परिवार पिता के नाम पर ही चलता है। पिता के वंश का नाम पुत्र को मिलता है।
प्रश्न 114.
मात-वंशी परिवार क्या है?
अथवा
मातृसत्तात्मक परिवार क्या है?
अथवा
मातृ-वंशी परिवार की परिभाषा दो।
उत्तर:
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि परिवार में सत्ता या शक्ति माता के हाथ ही होती है। बच्चों पर माता के रिश्तेदारों का अधिकार अधिक होता है न कि पिता के रिश्तेदारों का। स्त्री ही मूल पूर्वज मानी जाती है। संपत्ति का वारिस पत्र नहीं बल्कि माँ का भाई या भांजा होता है। परिवार माँ के नाम से चलता है। इस प्रकार के परिवार भारत में कुछ कबीलों में जैसे गारो, खासी आदि में मिल जाता है।
प्रश्न 115.
प्रतिबंधित बहु-पत्नी विवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर:
इस प्रकार के विवाह में पत्नियों की संख्या सीमित कर दी जाती है। वह एक बंधित सीमा से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। मुसलमानों में प्रतिबंधित बहु-पत्नी विवाह आज भी प्रचलित है जिसके अनुसार एक व्यक्ति के लिए पत्नियों की संख्या ‘चार’ तक निश्चित कर दी गई है।
प्रश्न 116.
अप्रतिबंधित बहु-पत्नी विवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर:
इस प्रकार के विवाह में पत्नियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती जितनी मर्जी चाहे पत्नियां रख सकता है। भारत में प्राचीन समय में इस प्रकार का विवाह प्रचलित था। जब राजा महाराजा बिना गिनती के पत्नियां या रानियां रख सकते थे।
प्रश्न 117.
मातृ-सत्तात्मक परिवार कौन-सा होता है?
उत्तर:
वह परिवार जहां सारे अधिकार माता के हाथ में होते हैं, परिवार माता के नाम पर चलता है तथा परिवार पर माता का नियंत्रण होता है, उसे मात-सत्तात्मक परिवार कहते हैं।
प्रश्न 118.
विवाह के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं?
उत्तर:
विवाह के आधार पर परिवार तीन प्रकार के होते हैं-
- एक विवाही परिवार
- बहु विवाही परिवार
- समूह विवाही परिवार।
प्रश्न 119.
बहु विवाही परिवार कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर:
बहु विवाही परिवार दो प्रकार के होते हैं-
- बहु पत्नी विवाही परिवार
- बहु पति विवाही परिवार।
प्रश्न 120.
नातेदारी क्या होती है?
अथवा
नातेदारी क्या है?
अथवा
नातेदारी किसे कहते हैं?
उत्तर:
नातेदारी समाज से मान्यता प्राप्त संबंध है जो अनुमानित या वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। नातेदारी का दूसरा नाम रिश्तेदारी भी है।
प्रश्न 121.
नातेदारी कितने प्रकार की होती है?
उत्तर:
नातेदारी दो प्रकार की होती है-
- रक्त मूलक या रक्त संबंधी नातेदारी।
- विवाह मूलक या विवाह से बनी नातेदारी।
प्रश्न 122.
संयुक्त परिवार के लाभों का वर्णन करो।
उत्तर:
- संयुक्त परिवार भूमि बंटने से बचाता है।
- संयुक्त परिवार श्रम विभाजन करता है।
- संयुक्त परिवार में खर्च में बचत हो जाती है।
प्रश्न 123.
संयुक्त परिवार के दोषों का वर्णन करो।
उत्तर:
- संयुक्त परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है।
- संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है।
- संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह आम रहती है।
प्रश्न 124.
संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन करो।
उत्तर:
- संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है।
- संयुक्त परिवार के कर्ता अर्थात् पिता की प्रधानता होती है।
- संयुक्त परिवार में संपत्ति, निवास तथा रसोई संयुक्त होती है।
प्रश्न 125.
एकाकी अथवा केंद्रीय परिवार के दो कार्य बताएं।
उत्तर:
- घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति आकर अपनी थकावट दूर कर सकता है। विवाह के बाद अपना घर बनाना तथा उसकी व्यवस्था करना केंद्रीय परिवार का मुख्य कार्य है।
- केंद्रीय परिवार अपने सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं तथा रहन-सहन के ढंगों को अपनी नई पीढ़ी को ठीक तरह से बताता है तथा सिखाता है।
प्रश्न 126.
केंद्रीय परिवार तथा संयुक्त परिवार में दो मुख्य अंतर बताएं।
अथवा
एकल परिवार और संयुक्त परिवार की तुलना करें।
उत्तर:
| संयुक्त परिवार | केंद्रीय परिवार |
| (1) संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर की होती है । वे पूर्ण रूप से आदमियों के अधीन होती हैं। | (1) केंद्रीय परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान होती है। परिवार में प्यार व समानता और मित्रता वाले संबंध मिलते हैं। |
| (2) संयुक्त परिवार में कर्त्ता का निरंकुश शासन चलता है। प्रत्येक निर्णय वही लेता है और शेष सदस्य उसका पालन करते हैं। | (2) केंद्रीय परिवार में महत्त्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में सभी की राय ली जाती है। सभी को अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार होता है। |
प्रश्न 127.
वर्ग निर्धारण के कौन-से आधार हैं?
उत्तर:
वर्ग निर्धारण के बहुत से आधार हैं जैसे कि पैसा, संपत्ति, शिक्षा, रहने का स्थान, पेशा, निवास स्थान की अवधि, व्यवसाय की प्रकृति, धर्म, परिवार तथा नातेदारी।
प्रश्न 128.
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु – – – वर्ष है?
उत्तर:
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
प्रश्न 129.
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु – – – – वर्ष है।
उत्तर:
हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
प्रश्न 130.
सामान्यतः संयुक्त तथा केंद्रक में से कौन-से परिवार की सदस्य संख्या अधिक होती है?
उत्तर:
सामान्यतः संयुक्त परिवार की सदस्य संख्या अधिक होती है।
प्रश्न 131.
………………… देश में विश्व की सबसे जटिल जाति व्यवस्था पाई जाती है।
उत्तर:
भारत देश में विश्व की सबसे जटिल जाति व्यवस्था पाई जाती है।
प्रश्न 132.
परिवार तथा नातेदारी में से कौन-सी वृहद (बड़ी) है?
उत्तर:
परिवार तथा नातेदारी में से नातेदारी बड़ी है।
प्रश्न 133.
किसी एक सामाजिक संस्था का नाम बताएँ।
उत्तर:
परिवार एक सामाजिक संस्था है।
प्रश्न 134.
विशेष विवाह अधिनियम कब पास हुआ?
उत्तर:
विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पास हुआ था।
प्रश्न 135.
किसी एक सामाजिक संस्था का नाम लिखें।
उत्तर:
विवाह, परिवार सामाजिक संस्थाएं हैं।
प्रश्न 136.
सामान्य संपत्ति किस परिवार की विशेषता है?
उत्तर:
सामान्य संपत्ति संयुक्त परिवार की विशेषता है।
प्रश्न 137.
जाति एक बंद ……………….. है।
उत्तर:
जाति एक बंद वर्ग है।
प्रश्न 138.
जाति व्यवस्था ……………….. पर आधारित है।
उत्तर:
जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है।

प्रश्न 139.
जाति एक नवीनतम सांस्कृतिक संस्थान है। (हां/नहीं)।
उत्तर:
नहीं।
प्रश्न 140.
जाति व्यवस्था व्यक्तियों को किस आधार पर वर्गीकृत करती है?
उत्तर:
जाति व्यवस्था व्यक्तियों को पेशे व जन्म के आधार पर वर्गीकृत करती है।
प्रश्न 141.
खंडात्मक संगठन क्या है?
उत्तर:
जो संगठन अलग-अलग खंडों या टुकड़ों में किसी आधार पर विभाजित हों उन्हें खंडात्मक संगठन कहा जाता है।
प्रश्न 142.
वर्गों को क्रम से लिखिए।
उत्तर:
- ब्राह्मण
- क्षत्रिय
- वैश्य, तथा
- शुद्र।
प्रश्न 143.
जनजातियों को कितने भाषायी परिवारों में बाँटा गया है?
उत्तर:
दो आधारों पर-स्थायी विशेषक तथा अर्जित विशेषक।
प्रश्न 144.
जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा अनूठा संस्थान है। (सत्य/असत्य)
उत्तर:
सत्य।
प्रश्न 145.
शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से जनजातियों का वर्गीकरण किन-किन श्रेणियों में किया गया है?
उत्तर:
शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से जनजातियों के लोगों को नीग्रिटो, आर्टेलॉयड, द्रविड तथा आर्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
प्रश्न 146.
पत्नी स्थानिक परिवार कौन-सा है?
उत्तर:
जब विवाह के पश्चात पति-पत्नी के घर रहने के लिए चला जाता है तो इसे पत्नी स्थानिक परिवार कहते हैं।
लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
पदक्रम क्या होता था?
उत्तर:
जाति प्रणाली में एक निश्चित पदक्रम होता था। भारत वर्ष में ज्यादातर भागों में ब्राह्मण वर्ण की जातियों को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था, इसी प्रकार दूसरे क्रम में क्षत्रिय आते थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जैसा तीसरा स्थान ‘वैश्यों’ का था। इसी क्रम के अनुसार सबसे बाद वाले क्रम में चौथा निम्न जातियों का था। समाज में किसी भी व्यक्ति की स्थिति भारत के ज्यादा भागों में उसी प्रकार से ही निश्चित की जाती थी। ब्राह्मणों को ज़्यादा आदर व सत्कार दिया जाता था और निम्न वर्ग भाव व्यक्तियों से दुर्व्यवहार होता है।
प्रश्न 2.
जाति का अलग-अलग हिस्सों में विभाजन होता था। व्याख्या करें।
अथवा
खंडात्मक संगठन क्या है?
उत्तर:
जाति प्रथा ने भारतीय सामाजिक ढांचे को अथवा भारतीय समाज को कई हिस्सों में बांट दिया है, सामान्यतः इसके चार भाग ही माने जाते हैं। इस प्रकार से इन चारों भागों में सबसे पहले भाग में ‘ब्राह्मण’ आते थे। दूसरे भाग में क्षत्रिय आते थे। इसके बाद वाला भाग वैश्यों को मिला था और आखिर वाला तथा चौथा भाग निम्न जातियों का माना गया था। इस तरह से हर खंड अथवा हिस्से का समाज में अपना-अपना दर्जा था। उसी प्रकार समाज में उनका स्थान, स्थिति अथवा कार्य प्रणाली थी, जिसमें उनको अपने रीति-रिवाजों के अनुसार चलना था। इसके अनुसार जाति के सदस्यों को अपने संबंधों का दायरा भी अपनी जाति तक ही सीमित रखना होता था। इस व्यवस्था में हर जाति अपने आप में एक संपूर्ण जीवन बिताने की एक ‘सामाजिक इकाई’ मानी जाती थी।
प्रश्न 3.
जाति के कार्यों का वर्णन करें।
अथवा
जाति का एक प्रकार्य बताइए।
उत्तर:
जाति व्यवस्था की प्रथा में जाति भिन्न तरह से अपने सदस्यों की सहायता करती है, उसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-
- जाति व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण करती है।
- व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- व्यक्ति एवं जाति के रक्त की शुद्धता बरकरार रखती है।
- जाति राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है।
- जाति अपने तकनीकी रहस्यों को गुप्त रखती है।
प्रश्न 4.
जाति सामाजिक एकता में रुकावट थी। कैसे?
उत्तर:
इस व्यवस्था से क्योंकि समाज का विभाजन कई भागों में हो जाता है, इसलिए सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति के अपने नियम एवं प्रतिबंध होते थे। इस तरह से अपनी जाति के अतिरिक्त दूसरी जाति से कोई ज्यादा लगाव नहीं होता क्योंकि उन्हें पता होता था कि उन्हें नियमों के अनुसार आचरण करना होता था।
इस प्रथा में हमेशा उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते थे। जाति भेद होने के कारण एक-दूसरे के प्रति नफरत की भावना भी उजागर हो जाती थी। यह भेदभाव समाज की एकता में बाधक बन जाता था। और इस व्यवस्था की यह कमी थी, कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर भी अपनी जाति को बदल नहीं सकता था। यह सामाजिक ढांचे का संतुलन बिगाड़ देती है और यह समाज की उन्नति में बाधक बन जाती थी।
प्रश्न 5.
जाति व्यवस्था के लाभों के बारे में बताएं।
उत्तर:
जाति व्यवस्था के लाभ निम्नलिखित हैं-
(i) हिंदू समाज का बचाव-जाति व्यवस्था ने मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमणों के समय हिंदू समाज की रक्षा की थी। यदि जाति व्यवस्था में विवाह, खाने-पीने तथा अन्य प्रतिबंध न होते तो हिंदू समाज मुसलमानों में मिल गया होता।
(ii) व्यवसाय निश्चित करना-जाति व्यवस्था ने हमेशा से ही हर जाति के व्यवसाय निश्चित किए हैं। ब्राहमण. क्षत्रिय, वैश्यों तथा निम्न जातियों के काम हमेशा उनकी जाति जन्म से ही निश्चित हो जाते थे। इससे हर किसी को काम मिल जाता था।
(iii) धार्मिक आधार बनाना-जाति व्यवस्था ने हमेशा समाज को धार्मिक आधार भी दिया है। प्रत्येक जाति के धार्मिक कर्तव्य निश्चित होते थे कि किस जाति ने किस प्रकार के धार्मिक संस्कारों का पालन करना है।
(iv) सामाजिक स्थिरता प्रदान करना-जाति व्यवस्था ने समाज को स्थिरता भी प्रदान की है। प्रत्येक जाति के काम, उसकी स्थिति, रुतबा निश्चित हुआ करता था। उच्च तथा निम्न जाति के बीच एक प्रकार का संबंध बना रहता था जिससे उनके संबंध स्थिर रहते थे तथा समाज में भी स्थिरता रहती थी।
प्रश्न 6.
जाति प्रथा की हानियों का वर्णन करें।
उत्तर:
जाति प्रथा की हानियों का वर्णन निम्नलिखित है-
(i) समाज को बांट देना-जाति प्रथा ने समाज को कई भागों में बांट दिया है। इस कारण इन जातियों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो गई तथा उनमें दुश्मनी भी हो गई। इस तरह समाज में नफरत फैलाने में जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है।
(ii) व्यक्तिगत विकास में बाधा-जाति व्यवस्था हर किसी का पेशा निश्चित कर देती है। चाहे कोई व्यक्ति अपनी जाति का काम करना चाहता हो या न उसे वह काम करना ही पड़ता था। जाति व्यवस्था व्यक्तिगत योग्यता में बहुत बड़ी बाधक है।
(iii) समाज के विकास में रुकावट-जाति प्रथा समाज के विकास में रुकावट है। हर कोई अपनी जाति, अपने लोगों के उत्थान के बारे में सोचता है। कोई समाज के विकास में ध्यान नहीं देता। इस तरह जाति समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधक है।
(iv) समाज सुधार में बाधक-जाति प्रथा के कारण निम्न जाति, शूद्र, अस्पृश्यता इत्यादि संकल्प हमारे सामने आए हैं। इसने निम्न जातियों के लोगों को नीचा ही रखा, उनको ऊपर नहीं आने दिया। इस तरह समाज सुधार में जाति प्रथा एक बाधक है।
(v) लोकतंत्र की विरोधी-जाति प्रथा लोकतंत्र की विरोधी है। लोकतंत्र समानता, भाईचारे तथा स्वाधीनता के विचारों का समर्थक है बल्कि जाति प्रथा में इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है।
प्रश्न 7.
जाति प्रथा ने हमारे समाज को किस तरह प्रभावित किया है?
उत्तर:
- जाति प्रथा ने सामाजिक गतिशीलता को चोट पहुँचायी है। व्यक्ति अपने पेशे के कारण से अपनी जगह छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता।
- जाति प्रथा ने समाज तथा व्यक्ति के आर्थिक विकास में भी रुकावट डाली है क्योंकि ऊँची जाति के व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्तियों के साथ काम करना पसंद नहीं करते।
- जाति प्रथा व्यक्तिगत कुशलताओं को बाहर नहीं आने देती।।
- आजकल राजनीति में जातिगत वोटों का बोलबाला है क्योंकि सभी अपनी ही जाति के लोगों से वोट मांगते हैं।
- जाति के राजनीति में आने से विभिन्न जातियों में दुश्मनी बढ़ी है।
- जाति प्रथा सांप्रदायिक दंगों के लिए भी कई बार कारण बन जाती है।
प्रश्न 8.
औद्योगीकरण ने जाति प्रथा को किस तरह प्रभावित किया है?
उत्तर:
- औद्योगीकरण के कारण बड़े-बड़े नगर बस गए जहां लोग बिना किसी भेदभाव के रहने लगे।
- औद्योगीकरण से पैसा बढ़ा जिससे जाति व्यवस्था के स्थान वर्ग व्यवस्था सामने आयी है।
- औद्योगीकरण से देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ोत्तरी हुई जिससे लोग, जाति तथा देश छोड़कर अन्य देशों में बसना शुरू हो गए।
- औद्योगीकरण के कारण लोग फैक्टरियों में मिलकर काम करने लगे जिससे अस्पृश्यता की भावना को धक्का लगा।
- इसके कारण से लोगों ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की जिससे उनके विचार उदारवादी हो गए।
प्रश्न 9.
जाति प्रथा में कौन-कौन से परिवर्तन आ रहे हैं?
अथवा
जाति प्रथा में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं?
उत्तर:
पुराने समय में जो कुछ भी जाति प्रथा का आधार था उन सभी में आजकल परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे कि-
- आजकल लोग जाति से बाहर विवाह कर रहे हैं।
- आजकल खाने-पीने के प्रतिबंध कोई नहीं मानता।
- ब्राह्मणों की प्रभुता काफी सीमा तक खत्म हो गई है।
- आजकल व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है।
- अस्पृश्यता को कानून की सहायता से खत्म कर दिया गया है।
प्रश्न 10.
विवाह की कोई चार विशेषताओं के बारे में बताओ।
उत्तर:
विवाह की चार विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
1. यौन संबंधों को नियमित करना-विवाह की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह स्त्री-पुरुष के यौन संबंधों को नियमित करता है। विवाह के बाहर यौन संबंधों को गैर-कानूनी करार दिया जाता है। इसलिए यौन संबंध निश्चित तथा नियमित करना विवाह का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।
2. संतान पैदा करना-विवाह की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि इससे संतान पैदा होती है। समाज की नियमितता तथा समाज के चलते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि पीढ़ी आगे बढ़े। अगर पीढ़ी आगे बढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए संतान पैदा करना विवाह का एक और उद्देश्य है।
3. परिवार की स्थापना-समाज बहुत सारे परिवारों का एक समूह है। विवाह के बाद पति-पत्नी परिवार का निर्माण पूरा करते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद परिवार पूरा हो जाता है। इस तरह विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण हो पाता है जोकि समाज के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है।
4. बच्चों का पालन-पोषण-विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है जहां बच्चे पैदा होते हैं तथा उनका पालन-पोषण होता है। विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चों का पालन-पोषण न तो अच्छी तरह हो पाता है तथा न ही उन्हें पिता तथा परिवार का नाम मिल पाता है। इस तरह विवाह से पैदा हुए बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह हो जाता है।
प्रश्न 11.
परिवार की कोई चार विशेषताएं बताओ।
उत्तर:
1. पति-पत्नी में संबंध-परिवार पति-पत्नी तथा उनके बच्चों से मिलकर बनता है। इस तरह पति-पत्नी के बीच किसी न किसी प्रकार के स्थायी संबंध परिवार की मुख्य विशेषता है। प्रत्येक संस्कृति में यह संबंध स्थायी होते हैं।
2. स्थायी लिंग संबंध-वैवाहिक संबंध के आधार पर परिवार का जन्म होता है। ये संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इन संबंधों के आधार पर पति-पत्नी में लिंग संबंध से संतान उत्पन्न होती है जिनको मान्यता प्राप्त होती है।
3. रक्त संबंधों का बंधन-परिवार की एक और विशेषता यह है कि परिवार के सदस्यों में रक्त संबंधों का होना है। ये रक्त संबंध वास्तविक भी हो सकते हैं तथा काल्पनिक भी। परिवार के सदस्य समान पूर्वज की संतान होते हैं।
4. सदस्यों के पालन-पोषण की आर्थिक अवस्था-परिवार में उसके सदस्य. बच्चों. बढों. स्त्रियों आदि के पालन पोषण की आर्थिक अवस्था होती है। परिवार के कमाने वाले सदस्य अन्य सदस्यों के पालन-पोषण का ज़रूरी प्रबंध करते हैं। इस तरह परिवार के सदस्य अधिकार तथा कर्तव्य के बंधनों में बंधे हए होते हैं।
प्रश्न 12.
परिवार के कार्यों का वर्णन करो।
उत्तर:
1. जैविक कार्य-
- संतान की उत्पत्ति
- सदस्यों की सुरक्षा
- भोजन, आवास तथा कपड़े की व्यवस्था
- बच्चों की सुरक्षा तथा देखभाल।
2. आर्थिक कार्य-
- श्रम विभाजन
- आय का प्रबंध
- संपत्ति की देखभाल।
3. सामाजिक कार्य-
- स्थिति को निश्चित करना
- समाजीकरण
- सामाजिक नियंत्रण
- सामाजिक विरासत का संग्रह तथा विस्तार।
4. धार्मिक शिक्षा प्रदान करना।
5. बच्चों के मनोरंजन संबंधी कार्य।
6. राजनीतिक कार्य-बच्चों को अधिकारों तथा कर्तव्यों का पाठ पढ़ाना।
प्रश्न 13.
निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है?
उत्तर:
निवास के आधार पर परिवार तीन प्रकार के होते है-
1. पितृ स्थानीय परिवार-जब विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर जाकर रहने लग जाती है तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं।
2. मातृ स्थानीय परिवार-जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लग जाए तो उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। यह पितृ स्थानीय परिवार के बिल्कुल उलट है।
3. नवस्थानीय परिवार-जब विवाह के पश्चात् पति-पत्नी किसी के घर न जाकर अपना नया घर बसाते हैं तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं।
प्रश्न 14.
नातेदारी के कितने प्रकार पाए जाते हैं?
अथवा
रक्तमूलक नातेदारी क्या है?
अथवा
रक्तमूलक नातेदारी किसे कहते हैं?
उत्तर:
नातेदारी के दो प्रकार पाए जाते हैं-
1. समरक्त संबंधी-रक्त या प्रजनन के आधार पर जो संबंधी पाए जाएं, उन्हें समरक्त संबंधी कहते हैं, जैसे माता-पिता का अपने बच्चों के साथ संबंध। माता, पिता, भाई, बहन के साथ संबंध इसी श्रेणी में आता है। यह संबंध सामाजिक मान्यताओं तथा जैविक तथ्यों पर आधारित होते हैं।
2. विवाह संबंधी नातेदारी-वह संबंध जोकि विवाह होने के पश्चात् बनते हैं, वह विवाह संबंधी नातेदारी होती है। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि केवल पति-पत्नी ही इस श्रेणी में नहीं आते बल्कि लड़का-लड़की के रिश्तेदारों के जो संबंध बनते हैं, वह भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि दामाद, जीजा, साला, साली, ननद, बहू इत्यादि।
प्रश्न 15.
नातेदारी संबंधों का क्या महत्त्व होता है?
अथवा
नातेदारी का समाज में क्या महत्त्व है?
उत्तर:
- नातेदारी संबंधों से परिवार में सत्ता का निर्धारण होता है।
- नातेदारी संबंधों से विवाह के समय काफी मदद मिलती है। कौन किस खानदान से है, कौन उसका रिश्तेदार है, यह काफ़ी महत्त्वपूर्ण होता है।
- हिंदू जीवन के धार्मिक संस्कारों तथा कर्मकांडों को पूरा करने के लिए नातेदारों, रिश्तेदारों की बहुत जरूरत होती है।
- व्यक्ति के जीवन में बहुत से सुख-दुःख आते हैं। उस समय सबसे ज्यादा ज़रूरत नातेदारों की पड़ती है।
प्रश्न 16.
कबीला अथवा जनजाति का क्या अर्थ है?
उत्तर:
कबीला अथवा जनजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हमारी सभ्यता से दूर पहाड़ों, जंगलों, घाटियों इत्यादि में आदिम तथा प्राचीन अवस्था में रहता है। यह समूह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहता है जिसकी अपनी ही अलग भाषा, अपनी संस्कृति, अपना ही धर्म होता है। ये समूह अंतर्वैवाहिक समूह होते हैं तथा प्यार, पेशे तथा उद्योगों के विषय में कुछ नियमों की पालना करते हैं। ये लोग हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा समाज से बिल्कुल ही अलग होते हैं। अलग-अलग कबीले अपनी सामाजिक संरचना, भाषा, संस्कृति इत्यादि जैसे कई पक्षों के आधार पर एक-दूसरे से अलग होते हैं।
प्रश्न 17.
कबाइली समाज किसे कहते हैं?
उत्तर:
कबीला एक ऐसा समूह है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति से दूर पहाड़ों, जंगलों, घाटियों इत्यादि में आदिम तथा प्राचीन अवस्था में रहता है। इन कबीलों में पाए जाने वाले समाज को कबाइली समाज कहा जाता है। कबाइली समाज वर्गहीन समाज होता है। इसमें किसी प्रकार का स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। प्राचीन समाजों में कबीले को बहुत ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह माना जाता था।
कबाइली समाज की अधिकतर जनसंख्या पहाड़ों अथवा जंगली इलाकों में पाई जाती है। यह समाज साधारणतया स्वःनिर्भर होते हैं जिनका अपने ऊपर नियंत्रण होता है तथा यह किसी के भी नियंत्रण से दूर होते हैं। कबाइली समाज, शहरी समाजों तथा ग्रामीण समाजों की संरचना तथा संस्कृति से बिल्कुल ही अलग होते हैं।
प्रश्न 18.
सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार के रूप में वर्ग तथा जाति में चार अंतर बताएं।
अथवा
जाति तथा वर्ग में दो अंतर बताइए।
अथवा
वर्ग और जाति में अंतर करें।
उत्तर:
| वर्ग | जाति |
| (i) वर्ग की सदस्यता व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर होती है। | (i) जाति की सदस्यता जन्म पर निर्भर होती है। |
| (ii) वर्ग में हम एक-दूसरे के वर्ग में विवाह कर सकते हैं। | (ii) जाति में हम दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। |
| (iii) वर्ग में सामाजिक संबंधों तथा खाने-पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। | (iii) जाति में जातियों में संबंधों तथा खाने-पीने संबंधी पाबंदियां होती हैं। |
| (iv) व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। | (iv) व्यक्ति का पेशा उसके वंश या जाति के अनुसार होता है। |
| (v) व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता से अपना वर्ग बदल सकता है। | (v) व्यक्ति चाह कर भी या योग्यता रखते हुए भी अपनी जाति नहीं बदल सकता। |
| (vi) वर्ग के कई आधार जैसे कि धन, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि होते हैं। | (vi) जाति का आधार केवल जन्म होता है। |
| (vii) वर्ग की कोई पंचायत नहीं होती। | (vii) जाति की अपनी जाति पंचायत होती है। |
| (viii) वर्ग में व्यक्तिगत योग्यता की प्रधानता होती है। | (viii) जाति में व्यक्तिगत योग्यता का कोई मूल्य नहीं होता केवल आपके परिवार तथा जाति का महत्त्व होता है। |
प्रश्न 19.
आज के समय में जाति व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करें।
उत्तर:
अगर आज के सामाजिक परिदृश्य को ध्यान से देखा जाए तो हमारे देश में जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। अब इस बात का कोई महत्त्व नहीं रह गया है कि वह किस समूह से संबंध रखता है। जाति व्यवस्था की संरचनात्मक व्यवस्था भी कमजोर हो रही है। जातीय भेदभाव, धार्मिक निषेध, जातीय मेल-जोल की पांबदियां खत्म हो रही हैं। अब जाति का व्यवसाय के साथ कोई संबंध नहीं रह गया है।
गांवों की जजमानी व्यवस्था भी खत्म हो रही है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्यक समूहों का दबदबा है न कि जातीय समूहों का। चाहे वैवाहिक क्षेत्र में जाति व्यवस्था का कुछ प्रभाव देखने को मिल जाता है, परंतु फिर भी प्राचीन समय वाला प्रभाव खत्म हो गया है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने इसे काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया है।
प्रश्न 20.
जनजातीय पहचान (Tribal Identity) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
जनजातीय पहचान का अर्थ है जनजातियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखना ताकि बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आने से उनकी संस्कृति का अस्तित्व खत्म न हो जाए। आजकल जनजातियां अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रही हैं जिस कारण ही जनजातीय पहचान का मुद्दा सामने आया है।
जनजातीय समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव, शिक्षा के प्रसार के कारण लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, संस्कृति को भूल रहे हैं, लोग आधुनिक बन रहे हैं। इससे उनकी मूल संस्कृति नष्ट हो रही है। इस कारण ही उनमें जनजातीय पहचान की चेतना उत्पन्न हो रही है ताकि उनकी विशेष संस्कृति, धर्म, भाषा इत्यादि को बचा कर रखा जा सके।
प्रश्न 21.
नातेदारी की श्रेणियों के बारे में बताएं।
अथवा
नातेदारी के दो प्रकार बताइये।
उत्तर:
नातेदारी की श्रेणियों को निकटता की मात्रा के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है-
(i) प्राथमिक नातेदारी-आमने-सामने की प्रत्यक्ष नातेदारी को प्राथमिक नातेदारी कहते हैं। यह 8 प्रकार की होती हैं जैसे कि पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बहन, माता-पुत्र इत्यादि।
(ii) द्वितीयक नातेदारी-जो नातेदारी प्राथमिक नातेदारों के द्वारा बने उसे द्वितीयक नातेदारी कहते हैं। जैसे कि पिता का भाई चाचा, माता का भाई मामा इत्यादि। इनके साथ हमारा संबंध प्राथमिक नातेदारों द्वारा बनता है। यह 33 प्रकार के होते हैं।
(iii) तृतीयक नातेदारी-जो नातेदारी द्वितीयक नातेदारों द्वारा बनती है उसे तृतीयक नातेदारी कहते हैं। जैसे कि पिता के भाई की पत्नी चाची, माता के भाई की पत्नी मामी इत्यादि। यह 151 प्रकार के होते हैं।
प्रश्न 22.
परिहास प्रथा क्या है?
उत्तर:
परिहास या हँसी मज़ाक के संबंधों में हँसी मज़ाक, यौन संबंधी अश्लील कथन, गाली गलौच इत्यादि का समावेश होता है। इस प्रकार के संबंधों में स्वतंत्रता पाई जाती है। इस प्रकार का व्यवहार आमतौर पर विवाह संबंधियों में मिलता है जैसे कि देवर-भावी, ननद-भाभी, जीजा-साली इत्यादि कई बार तो इस प्रकार के संबंधों में यौन संबंध तक स्थापित हो जाते हैं। एक विद्वान् के अनुसार कई बार तो इस प्रकार के संबंधों में इतनी घनिष्ठता आ जाती है कि वह विवाह तक कर लेते हैं।
निबंधात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है? इसकी विशेषताएं बताएं।
अथवा
जाति व्यवस्था की परिभाषा दीजिए।
अथवा
जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
अथवा
जाति की विशेषताएँ लिखें।
अथवा
जाति की परिभाषा देकर अर्थ बताएँ।
अथवा
जाति प्रथा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? विस्तार कीजिये।
अथवा
जाति व्यवस्था क्या है? जाति की सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएं कौन-सी हैं?
उत्तर:
जाति का अर्थ (Meaning of Caste System)-जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द CASTE का हिंदी रूपांतर है, जो कि पुर्तगाली शब्द CASTA से लिया गया है। CASTA एक पुर्तगाली शब्द है, जिसका अर्थ है नस्ल। इसी प्रकार शब्द CASTE का लातीनी भाषा के शब्द CASTUS से भी गहरा संबंध है, जिसका अर्थ शुद्ध नस्ल होता है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती थी। व्यक्ति को तमाम आयु उस जाति से संबंधित रहना पड़ता था जिस जाति में उसने जन्म लिया है। जब व्यक्ति जन्म लेता था उसी समय ही उसके जीवन जीने के ढंग निश्चित कर दिए जाते थे तथा उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। व्यक्ति पर जो भी प्रतिबंध जाति व्यवस्था द्वारा लगा दिए जाते हैं, उसके लिए उन्हें मानना आवश्यक होता था।
यह जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मूल आधारों में से एक है तथा हिंदू सामाजिक जीवन के लगभग सभी पहलू इससे प्रभावित हुए हैं। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली रहा है कि भारत में बसने वाले प्रत्येक समूह तथा समुदाय को इसने प्रभावित किया है।
जाति शब्द संस्कृत के शब्द ‘जन’ से लिया गया है जिसका अर्थ है ‘जन्म’। जाति शब्द अंग्रेजी के शब्द CASTE (कास्ट) का हिंदी रूपांतर है जो कि पुर्तगाली शब्द Casta से लिया गया है। चाहे ये और भी सामाजिक व्यवस्थाओं में भी पाया जाता है, परंतु भारत में इसका विकसित रूप ही नज़र आता है।
परिभाषाएं-जाति व्यवस्था की कई प्रमुख समाज शात्रिस्यों ने निम्नलिखित ढंग से परिभाषाएं दी हैं-
(1) रिज़ले (Risley) के अनुसार, “जाति परिवारों और परिवारों के समूह का संकल्प है’ जिसका इसके अनुरूप नाम होता है और वो काल्पनिक पूर्वज मनुष्य या दैवी के वंशज होने का दावा करते हैं जो समान पैतृक कार्य अपनाते हैं और वे विचारक जो इस विषय को ‘देव योग’ मानते हैं इसे ‘समजाति-समुदाय’ मानते हैं।”
(2) राबर्ट बीयरस्टेड (Robert Bierstdt) के अनुसार, “जब वर्ग प्रथा का ढांचा एक या अधिक विषयों पर पूरी तरह बंद होता है तो उसको ‘जाति प्रथा’ कहा जाता है।”
(3) बलंट (Blunt) के अनुसार, “जाति एक अंतर वैवाहिक समूह या अंतर वैवाहिक समूहों का इकट्ठ है जिसका एक नाम है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत है जोकि अपने सदस्यों के ऊपर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है, एक सामान्य परंपरागत पेशे को करती है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और आमतौर पर एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है।’
(4) मैकाइवर तथा पेज (Maclver and Page) के अनुसार, “जब स्थिति पूरी तरह पूर्व निश्चित होती हो व्यक्ति बिना किसी आशा को लेकर पैदा होते हों तो वर्ग जाति का रूप धारण कर लेती है।’
(5) जे० एच० हट्टन (J.H. Hutton) के अनुसार, “जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज एक आत्म केंद्रित तथा एक-दूसरे से पूर्ण रूप से अलग इकाइयों में बंटा रहता है। इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर संबंध उच्च निम्न के आधार पर तथा संस्कारों के आधार पर निर्धारित होते हैं।”
इस तरह इन परिभाषाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि जाति एक अन्तर्विवाहित समूह होता है। इस की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। पेशा परंपरागत होता है और जातियों के खाने-पीने तथा रहन-सहन की पाबंदी होती है तथा विवाह संबंधी कठोर पाबंदियां होती हैं।
जाति व्यवस्था की विशेषताएँ
1. सदस्यता जन्म के ऊपर आधारित है (Membership is based upon Birth) इस प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी जाति का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता, किसी की भी जाति उसके जन्म के आधार पर ही निश्चित की जाती है। जिस भी जाति में वह व्यक्ति जन्म लेता था उसी के अनुसार, उसकी जाति निश्चित हो जाती थी।
2. सामाजिक-संबंधों के ऊपर प्रतिबंध (Restrictions upon Social Relations) समाज को अलग-अलग जातियों में विभाजित किया गया था। कोई उच्च जाति से संबंध रखता था तो कोई निम्न जाति से। जाति प्रथा में इस भावना को तो पाया ही जाता था। उच्च जाति वाले हमेशा शहरों एवं गाँवों में रहते थे और निम्न जाति वालों को बाहर रहना पड़ता था। इस तरह निम्न जाति वाले अपने आपको ऊँची जाति वालों से दूर रखना या रहना ही ठीक समझते थे।
3. खाने-पीने पर प्रतिबंध (Restrictions upon Eatables}-जाति प्रणाली में यह बात स्पष्ट रूप से बतायी जाती थी कि व्यक्तियों को किन-किन वर्गों के लोगों के साथ उठना-बैठना होता था और किन-किन लोगों के साथ खाने-पीने पर प्रतिबंध था। इस प्रकार से भोजन को भी दो श्रेणियों में बांटा गया था जोकि दो तरह से तैयार होता था। नं० 1 भोजन जो कि घी द्वारा तैयार किया जाता था एवं पकाया जाता था, उसे पक्का भोजन कहा गया है और उसे ब्राह्मणों द्वारा तैयार किया जाता या उसके गुरु द्वारा तैयार किया जाता था।
इसी प्रकार कच्चा भोजन, जोकि पानी द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार यदि ब्राह्मण वर्ग द्वारा कच्चा भोजन भी तैयार किया जाता था, तो दूसरी जाति के लोग उसे ग्रहण कर लेते थे परंतु दूसरी जातियों द्वारा तैयार कच्चा भोजन ब्राह्मण कभी भी ग्रहण नहीं करते थे। ब्राह्मण लोग, क्षत्रियों एवं वैश्यों द्वारा पकाया हुआ भोजन स्वीकार कर लेते थे।
4. व्यवसाय अपनाने हेतु पाबंदियां (Restrictions upon Occupation)-जाति प्रथा में विशेष, परंपरागत धंधों को अपनाया जाता था। यदि किसी जाति का कोई विशेष व्यवसाय होता था तो उसे वही पेशा ही अपनाना पड़ता था। इस प्रकार व्यक्ति के पास कोई पसंद या पहल यानि की कोई Choice नहीं होती थी अर्थात् वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था।
परंतु इसमें कुछ धंधों में जैसे कि व्यापार, खेतीबाड़ी और सुरक्षा के मामलों में, नौकरी संबंधी कई विभागों में वह अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करने के भी प्रावधान थे। कई समूहों को कोई भी पेशा अपनाने की छूट थी। परंतु कई जाति-समूहों जैसे की लोहारों, बढ़ई, बारबर, कुम्हार इत्यादि को अपने परंपरागत कार्यों को ज्यादातर अपनाना पड़ता था।
इस प्रणाली में ब्राह्मणों को विशेष कार्य अर्थात् शिक्षा प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण कार्य मिला हुआ था। क्षत्रियों को सुरक्षा का जिम्मा मिला हुआ था। वैश्यों को खेतीबाड़ी, पशुपालन एवं व्यापार के लिए विकल्प खुले थे।
5. विवाह संबंधी पाबंदियां (Restrictions for Marriages)-जाति प्रथा में जातियों को इस तरह से विभाजित किया जाता था कि आगे उनकी उपजातियां भी बनाई गई थीं। इन उपजातियों में यह बंधन था कि अपने सदस्यों को दूसरी जाति में विवाह करने से रोकते थे। अपनी जाति के अंदर ही विवाह करने की प्रथा को जाति विशेष की विशेषता माना जाता था। इस प्रणाली में कुछ उपजातियों को दूसरी जातियों में भी विवाह का कुछ हालातों में किसी लड़की से विवाह कर सकते थे। परंतु यह आम नियम था कि एक व्यक्ति अपनी ही उपजाति में विवाह कर सकता था। इस प्रकार यदि वह नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे अपनी उपजाति में से बाहर निकाल दिया जाता था।
6. समाज का अलग-अलग हिस्सों में विभाजन (Segmantal Division of Society)-जाति प्रथा के अनुसार समाज को कई भागों में बांटा गया था और हर हिस्से के सदस्यों का दर्जा, स्थान और कार्य निश्चित कर दिये गये थे। इसलिए सदस्यों में अपने समूह का एक हिस्सा होने की चेतना पैदा होती थी अर्थात् वह अपने समूह का एक अटूट अंग बन जाते थे। समाज का इस तरह हिस्सों में बंट जाने के कारण एक जाति के सदस्यों का सामाजिक अंतर, कार्य का दायरा ज्यादातर अपनी जाति तक ही सीमित हो जाता था।
जाति के नियमों की पालना न करने वालों को जाति की पंचायत दंड भी दे सकती थी। भिन्न-भिन्न जातियों के रहन-सहन के ढंग और रस्मों-रिवाजों में भी अंतर होता था। एक ही जाति के लोग प्रायः अपनी ही जाति के लोगों से अंतर कार्य करते थे। हर जाति अपने आप में एक-एक संपूर्ण सामाजिक जीवन जीने वाली सामाजिक इकाई होती थी।
7. पदक्रम (Hierarchy)-जाति प्रथा में एक निश्चित पदक्रम होता था। भारत में ज़्यादातर सभी भागों में सबसे ऊपर का दर्जा ब्राह्मणों को दिया गया था। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को रखा गया था। तीसरे स्थान पर वैश्यों को और इसी सामाजिक पदक्रम में सबसे बाद में यानि कि चौथे स्थान पर निम्न जातियों को रखा गया था। इस तरह से समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति को पदक्रम के आधार पर निश्चित किया गया था।
8. प्रत्येक जाति कई उपजातियों में बंटी होती है (Every caste is divided into many sub-castes) हमारे देश में तीन हज़ार के लगभग जातियां पाई जाती हैं तथा यह सभी जातियां आगे बहुत-सी उपजातियों में बंटी हुई थीं। व्यक्ति को अपना जीवन इन उपजातियों के नियमों के अनुसार व्यतीत करना पड़ता था तथा व्यक्ति को केवल अपनी ही उपजाति में विवाह करवाना पड़ता था।
9. अंतर्वैवाहिक (Endogamous)-जाति प्रथा में विवाह से संबंधित बहुत-सी पाबंदियां थीं। व्यक्ति के ऊपर अपनी जाति से बाहर विवाह करवाने की पाबंदी थी। यही नहीं व्यक्ति को केवल अपनी ही उपजाति में विवाह करवाना पड़ता था। जो व्यक्ति जाति प्रथा के नियमों को तोड़ता था उसे साधारणतया जाति से बाहर ही निकाल दिया मजूमदार के अनुसार संस्कृति के संघर्ष तथा नस्ली मेल-मिलाप ने भारत में उच्च तथा निम्न दर्जे के समूहों की रचना की।
नस्ली मिश्रण के कई कारण थे जैसे आर्यों में स्त्रियों की कमी, उन्नत द्राविड़ संस्कृति, उनकी मात प्रधान व्यवस्था, देवी-देवताओं की पूजा, एक जगह पर जीवन व्यतीत करने की इच्छा, अलग-अलग रीति-रिवाज इत्यादि। आर्य लोगों द्वारा द्राविड़ लोगों को जीतने के पश्चात् उनमें आपसी मेल-मिलाप तथा सांस्कृतिक संघर्ष चलता रहा। इस कारण कई सामाजिक समहों का निर्माण हआ जो अंतर्विवाहित बन गए। यहां से प्रत्येक समह या जाति का दर्जा इस समूह की रक्त शुद्धता तथा दूसरे समूहों से अलग रहने के आधार पर निर्धारित हो गया।
नस्ली सिद्धांत की आलोचना होती है क्योंकि इस सिद्धांत ने वैवाहिक संबंधों पर रोक के बारे में तो बताया है परंतु खाने-पीने के नियमों का कोई वर्णन नहीं किया है। मुसलमान तथा ईसाई सांस्कृतिक भिन्नता होने के बावजूद भी जाति का रूप धारण नहीं कर सके हैं। इस तरह जाति प्रथा की उत्पत्ति कई कारणों के कारण हुई है केवल एक कारण की वजह से नहीं।
3. भौगोलिक सिद्धांत (Geographical Theory)-जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में भौगोलिक सिद्धांत गिलबर्ट (Gilbert) ने दिया है। उसके अनुसार जातियों का निर्माण अलग-अलग समूहों के देश के अलग-अलग भागों में बसने के कारण हुआ है। यह विचार तमिल साहित्य में भी दिया गया है। इस विचार की पुष्टि कई उदाहरणों के कारण होती है।
जैसे सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहलाए तथा कन्नौज में रहने वाले कनौजिए हो गए। इस तरह कई और जातियों के नाम भी उनके निवास स्थान के आधार पर पड़ गए। परंतु इस सिद्धांत को ज्यादातर विद्वानों ने नकार दिया है क्योंकि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में कई जातियां मिलती हैं परंतु उनमें से सभी के नाम उस क्षेत्र से संबंधित नहीं होते।
4. व्यावसायिक या पेशे से संबंधित सिद्धांत (Occupational Theory)-व्यवसाय के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत नेसफील्ड तथा डाहलमैन (Nesfield and Dahlman) ने दिया है। नेसफील्ड के अनुसार जातियों की उत्पत्ति अलग-अलग व्यवसायों के आधार पर हुई है तथा उसने नस्ली कारकों को नकार दिया है। जाति व्यवस्था के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही नस्ली मिश्रण बढ़ चुका था। उसके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति धर्म के कारण भी नहीं हुई है क्योंकि धर्म वह कट्टर आधार नहीं दे सकता जो जाति व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। इस तरह नेसफील्ड के अनुसार केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए ज़िम्मेदार है।
डाहलमैन के अनुसार शुरू में भारतीय समाज तीन भागों में बँटा हुआ था तथा वह थे-रोहित, शासक तथा बुर्जुआ। इन तीनों वर्गों के व्यवसाय धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाओं से संबंधित थे। इनके समूह व्यवसाय तथा रिश्तों के आधार पर छोटे-छोटे समूहों में बंट गए। यह पहले व्यावसायिक निगमों तथा धीरे-धीरे बड़े व्यावसायिक संघों का रूप धारण कर गए। आगे चल कर संघ जाति के रूप में विकसित हो गए।
की भी आलोचना हई है। जाति प्रथा का धर्म से कोई सीधा संबंध न बताना उचित नहीं है। यह सिद्धांत नस्ली सिद्धांतों से दूर है क्योंकि उच्च तथा निम्न सामाजिक समूहों में कुछ-न-कुछ नस्ली अंतर ज़रूर है। इसके साथ ही यदि जाति प्रथा की उत्पत्ति व्यावसायिक संघों के कारण ही हुई तो यह केवल भारत में ही क्यों आगे आई और देशों में क्यों नहीं। इस तरह इस सिद्धांत में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है।
5. विकासवादी सिद्धांत (Evolutionary Theory)-इस सिद्धांत को डैनज़िल इबैटस्न (Denzil Ibbetson) ने दिया है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति चार वर्णों के आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर बने संघों द्वारा हुई है। उसके अनुसार पहले लोग खानाबदोशों की तरह रहते थे तथा जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई थी। लोगों में खून का रिश्ता होता था तथा उच्च-निम्न की भावना नहीं थी।
परंतु धीरे-धीरे इकठे रहने से आर्थिक विकास शुरू हुआ तथा लोग कृषि कार्य करने लगे। समय के साथ-साथ आर्थिक जीवन के जटिल होने के कारण श्रम विभाजन की आवश्यकता महसूस हुई। राजाओं का यह कर्तव्य बन गया कि वह ऐसी आर्थिक नीति का निर्माण करें जोकि श्रम विभाजन तथा व्यावसायिक भिन्नता पर आधारित हो।
इस कारण कई नए वर्ग अस्तित्व में आए। एक जैसा कार्य करने के कारण सामुदायिक भावना का विकास हुआ। समय के साथ-साथ इन वर्गों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बना लिए। प्रत्येक संघ ने अपने भेदों को गुप्त रखने के लिए अंतर्विवाह की नीति अपनायी। इस तरह जाति वैवाहिक होने के कारण जाति प्रथा उत्पन्न हई। धीरे-धीरे इन समहों ने सामाजिक सामाजिक पदक्रम में अपना स्थान बना लिया।
इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है क्योंकि व्यवसाय के आधार पर संघ तो सभी समाजों में मिलते हैं पर केवल भारत में ही जाति प्रथा क्यों विकसित हुई। आर्थिक कारक को बहुत-से कारकों में से एक कारक तो माना जा सकता है पर केवल एक ही कारक नहीं।
6. धार्मिक सिद्धांत (Religious Theory)-इस सिद्धांत को होकार्ट तथा सेनार्ट ने दिया है। होकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तथा भारतीय समाज का विभाजन धार्मिक कर्मकांडों तथा सिद्धांतों के कारण हुआ है। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म बहुत महत्त्वपूर्ण था जिस में देवताओं को बलि भी दी जाती थी। बलि की प्रथा में पूजा पाठ तथा मंत्र पढ़ना शामिल था जिसमें कई व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी। धीरे-धीरे धार्मिक कार्य करने वाले लोग संगठित हो गए तथा उन्होंने अलग-अलग जातियों का रूप धारण कर लिया। होकार्ट के अनुसार प्रत्येक जाति का व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता है तथा व्यवसाय का मूल आधार धार्मिक है न कि आर्थिक।
सेनार्ट के अनुसार भोजन संबंधी प्रतिबंध धार्मिक कारणों के कारण पैदा हुए तथा लोग जातियों तथा उपजातियों में विभाजित हो गए। परंतु कई समाजशास्त्रियों के अनुसार जाति व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है न कि धार्मिक। इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं प्रतीत होता है। जाति व्यवस्था बहुत ही जटिल है परंतु इसकी उत्पत्ति का बहुत ही सरल वर्णन किया गया है जोकि ठीक नहीं है।
7. माना सिद्धांत (Mana Theory) हट्टन का कहना है कि आर्य लोगों के भारत आने से पहले भी जाति व्यवस्था के तत्त्व भारत में मौजूद थे। जब आर्य लोग भारत में आए तो उन्होंने इन तत्त्वों को अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ किया। उनसे पहले भारत में सामाजिक विभाजन ज्यादा स्पष्ट नहीं था परंतु आर्यों ने इसे अलग किया तथा अपने आपको इस व्यवस्था में सब से ऊपर रखा।
हट्टन का कहना था कि यह प्रारंभिक अवस्था थी। जाति व्यवस्था के प्रतिबंधों को उसने माना तथा टैबु की मदद से स्पष्ट किया है। प्राचीन समाजों में माना को अदृश्य आलौकिक शक्ति समझा जाता था जो कि प्रत्येक प्राणी में होती है तथा छूने से एक-दूसरे में भी आ सकती है।
कबीलों के लोग यह मानते हैं कि माना शक्ति के कारण ही लोगों में भिन्नता होती थी। माना के डर से ही यह लोग बाहर के व्यक्तियों से दूर रहते हैं। अपने समूहों में भी वह उन लोगों को नहीं छूते थे जिनको दुष्ट समझा जाता था। इस तरह कबीले के लोगों के बीच कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है जिनको टैबु कहते हैं। लोगों में यह डर होता था कि टैबु को न मानने वालों के ऊपर दैवी प्रकोप हो जाएगा।
हट्टन के अनुसार माना तथा टैबु को मानने वाले हिंदू, इस्लाम, पारसी तथ बुद्ध धर्म को मानने वालों में भी मिलते हैं। आर्य लोगों के आने से पहले भी भारत में माना तथा टैबु से संबंधित भेदभाव मिलते थे। इस कारण विवाह, खाने-पीने, कार्यों इत्यादि से संबंधित प्रतिबंध अलग-अलग समूहों में मिलते थे। इस कारण जब जाति व्यवस्था शुरू हुई तो उसमें कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गईं।
कई विद्वानों ने इस बात की आलोचना की है तथा कहा है कि चाहे माना, टैबु संसार के अन्य कबीलों में भी मिलते हैं परंतु हमें जाति व्यवस्था कहीं भी नहीं मिलती है। इसके साथ कबीलों की संस्कृति संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हट्टन ने कोई ऐसे तथ्य भी पेश नहीं किए जिस के आधार पर माना जा सके कि आर्य लोगों से पहले भी भारत में मूल निवासी माना तथा टैबु के आधार पर बँटे हुए थे।

प्रश्न 3.
जाति प्रथा के लाभों तथा हानियों का वर्णन करो।
अथवा
जाति व्यवस्था के कार्य अथवा लाभ स्पष्ट करें।
उत्तर:
जाति व्यक्ति, समुदाय तथा समाज के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करती है इसलिए यह संस्था सैंकड़ों वर्षों से भारतीय समाज का आधार रही है। जाति प्रथा के बहुत से लाभ तथा हानियां हैं जिन का वर्णन निम्नलिखित है
जाति प्रथा के लाभ (Advantages of Caste System)-
(i) सामाजिक स्थिति निर्धारित करना (Determining Social Status)-जाति अपने सदस्यों को जन्म से ही निश्चित स्थिति प्रदान करती थी। व्यक्ति शिक्षा. गरीबी-अमीरी, आय तथा लिंग या व्यक्तिगत योग्यता से अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकता था। जाति के आधार पर ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर तथा शेष की इनसे निम्न होती थी।
(ii) सरल श्रम विभाजन (Simple Division of Labour)-जाति प्रथा में श्रम विभाजन हुआ करता था। हर किसी को एक काम उसके परिवार तथा जाति के अनुसार मिल जाता था। विभिन्न जातियों द्वारा निश्चित कार्य करना समाज में श्रम विभाजन का अच्छा उदाहरण है। हर किसी को निश्चित कार्य देने के कारण समाज में श्रम विभाजन हो जाता था।
(iii) जीवन साथी चुनने में सहायक (Helpful in choosing Life Male)-जाति अंतर्विवाही होती है। इसलिए व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपनी जाति में ही विवाह करे। इससे जीवन साथी चुनने में सरलता हो जाती है।
(iv) व्यवसाय निर्धारित करना (To determine Occupation)-जातियों का अपना-अपना व्यवसाय होता है। इसके सदस्य अपनी जाति के अनुरूप व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है।
(v) रक्त की शुद्धता (Purity of Blood)-जाति अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह में नियमों पर आधारित है। अपनी जाति के अंदर विवाह करवाना तथा बहिर्विवाह का मतलब अपने सपिंड, सप्रवर तथा सगोत्र से बाहर विवाह करवाना होता है। इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है।
(vi) व्यवहारों पर नियंत्रण (Control on Behaviour)-प्रत्येक जाति के अपने मूल्य, प्रतिमान तथा नियम होते हैं। जाति नियम यह तय करते हैं कि किस जाति के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाएं। छूतछात, धर्म, खानपान, व्यवसाय इत्यादि संबंधी नियमों के द्वारा जाति अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है।
(vii) सामाजिक सुरक्षा (Social Security)-जाति अपने सदस्यों की स्थिति का निर्धारण करती है। जाति के सदस्य ज़रूरत पड़ने पर गरीबों, अनाथों, बच्चों तथा विधवाओं की सहायता करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
(viii) मानसिक सुरक्षा (Psychological Security)-जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। कई प्रकार के नियम जाति तय करती है। जातीय लोक रीतियां तथा प्रथाएं भी स्पष्ट होती हैं जिनके कारण व्यक्ति को मानसिक शांति व सुरक्षा का अहसास होता है।
(ix) सामाजिक स्थिरता (Social Stability)-भारत पर बहुतों ने आक्रमण किए। सैंकड़ों वर्ष विदेशियों ने यहां पर राज किया। इस विदेशी शासन के दौरान भी जाति प्रथा ने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा तथा सामाजिक स्थिरता प्रदान की।
जाति प्रथा की हानियां (Disadvantages of Caste System):
(i) निम्न जातियों का शोषण (Exploitation of Low Castes)-जाति प्रथा में निम्न जातियों का शोषण होता था। उनसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था जिसके बदले में पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। उनसे निम्न स्तर के घृणित कार्य करवाये जाते थे। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध हुआ करते थे। इस तरह उनका शोषण हुआ करता था।
(ii) अस्पृश्यता (Untouchability)- जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में अस्पृश्यता या छूतछात को जन्म दिया। कई क्षेत्रों में तो जाति का उग्र रूप भी देखने को मिलता था कि कुछेक निम्न जाति के लोगों की परछाईं मात्र से अन्य जाति के लोग अपने आप को दूषित समझते थे।
(iii) धर्म परिवर्तन (Religion Conversion)-निम्न जातियों को उनकी निम्न स्थिति का अहसास करवा कर मिशनरी धर्म प्रचारक उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उत्साहित करते हैं। समाज में उचित स्थान न मिलने के कारण निम्न जाति के सदस्य धर्म परिवर्तन कर लेते थे ताकि जाति व्यवस्था से छुटकारा मिल सके।
(iv) व्यक्तित्व विकास में बाधक (Hindrance in Personality Development)-जाति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। व्यक्ति योग्यता होते हुए भी अपना विकास नहीं कर सकते थे। व्यक्ति उच्चता तथा निम्नता की भावना से ग्रसत रहते हैं जिस के कारण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है।
(v) राष्ट्रीय एकता में बाधक (Hindrance in National Unity)-जाति के आधार पर समाज तथा समुदाय छोटे-छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। व्यक्ति की निष्ठा जाति के प्रति अधिक तथा राष्ट्र के प्रति कम हो जाती है। अपनी जाति के सदस्यों में हम की भावना रहती है जबकि अन्य जातियों के प्रति घृणा की भावना विकसित हो जाती है जिससे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इस तरह यह राष्ट्रीय एकता में बाधक है।
(vi) स्त्रियों की निम्न स्थिति (Low Status of Women)-जाति प्रथा द्वारा बाल विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह की मनाही तथा स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। जाति व्यवस्था में स्त्री की कोई जाति नहीं होती। वह जिस जाति के पुरुष से विवाह करती है उसी की जाति उसकी जाति बन जाती है। इन सबसे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न हो जाती है।
प्रश्न 4.
जाति प्रथा में आ रहे परिवर्तनों का वर्णन करें।
अथवा
जाति व्यवस्था में आये आधुनिक परिवर्तन स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
भारतीय जाति व्यवस्था में लगातार संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते रहे हैं। इन परिवर्तनों की गति स्थान तथा हालातों के अनुसार भिन्न-भिन्न रही है। आजादी के बाद जाति प्रथा में काफी तेज़ी से परिवर्तन आए हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है:
(i) उच्च जातियों की स्थिति में गिरावट (Decline in status of Brahmins)-जाति व्यवस्था की शुरुआत से ही उच्च जातियों का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्त्व रहा है। परी जाति व्यवस्था उनके इर्द-गिर्द घमती थी। जाति के संस्तंरण में उनका सर्वोच्च स्थान रहा है। परंतु शिक्षा के प्रसार, विज्ञान के विकास, नए पदों का सृजन, पश्चिमीकरण, संस्कतिकरण, आधनिकीकरण, नगरीकरण इत्यादि के कारण उनकी स्थिति में गिरावट आई है। आजकल गैर-ब्राहमणों की स्थिति उनकी शिक्षा, पैसे या सत्ता के कारण उच्च है। इस तरह उच्च जातियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई है।
(ii) अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन (Change in Inter Caste Relations)-प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था प्रचलित रही है जिसके चलते विभिन्न जातियों में अंतर्निर्भरता बनी रहती थी। परंतु अंतर्जातीय संबंधों में अब काफी परिवर्तन हुए हैं। पैसे के प्रचलन, उद्योगों के विकास तथा शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार के कारण विभिन्न जातियों ने अपने परंपरागत व्यवसाय छोड़ने शुरू कर दिए हैं। सेवाओं के आदान-प्रदान में भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। लोग पैसे देकर चमड़े, बांस, मिट्टी इत्यादि की चीजें खरीदने लग गए हैं। अच्छी चीजें उपलब्ध होने के कारण लोग बाज़ार जाने लग गए हैं। पढ़े-लिखे युवाओं द्वारा भी परंपरागत काम छोड़ने के कारण अंतर्जातीय संबंधों का स्वरूप बदला है।
(iii) अस्पृश्यता में कमी (Decline in Untouchability)-जाति प्रथा में अस्पृश्यता का बोलबाला था। पर आज़ादी के बाद इसमें कमी आयी है। औद्योगीकरण के कारण सभी जातियों के लोग मिल कर काम करते हैं। 1955 में अस्पृश्यता कानून भी पास हो गया जिसके अनुसार अस्पृश्यता को मानना गैर कानूनी है। होटलों, क्लबों में सभी को प्रवेश मिलने से अस्पृश्यता में काफी कमी आयी है। कानून की वजह से भी इसमें काफ़ी कमी आई है।
(iv) वैवाहिक परिवर्तन (Matrimonial Changes)-हिंदू विवाह कानून 1955 द्वारा अंतर्जातीय विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। अंतर्विवाह जाति प्रथा का सार रहा है। समाचार पत्रों में प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापनों में Caste No bar का लिखा होना इस बात का प्रमाण है कि अब लोगों में जाति में विवाह करवाना ज़रूरी नहीं रह गया है। अब प्रेम विवाह बढ़ रहे हैं जिससे पता चलता है कि वैवाहिक प्रतिबंध ढीले हो रहे हैं।
(v) जन्म के महत्त्व में कमी (Importance of Birth is Declining)-भारतीय समाज में पारंपरिक दृष्टि से व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसकी सामाजिक स्थिति उसी जाति के अनुसार ही हो जाती है। लेकिन आजकल व्यक्ति के जन्म के आधार पर स्थिति का महत्त्व कम होता जा रहा है। उसकी व्यक्तिगत योग्यता तथा कुशलता का महत्त्व बढ़ रहा है। आजकल व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समाज में जन्म से नहीं बल्कि गुणों तथा कर्मों तथा उपलब्धियों के कारण है। व्यक्ति को जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। जन्म के महत्त्व में कमी आने से जातीय आधार पर सामाजिक स्थिति के निर्धारण में परिवर्तन हुआ है।
(vi) व्यावसायिक गतिशीलता में वृद्धि (Increase in Occupational Mobility)-भारतीय समाज में जातिगत व्यवसायों में काफ़ी गतिशीलता आई है। बहुत सारे नए व्यवसायों का विकास हुआ है। लाखों नए पदों का विकास हुआ है। विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है इसलिए सभी ने शिक्षा लेनी शुरू की। शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई भी किसी भी पद का पात्र बन सकता है। निम्न जाति का सदस्य संस्कृत तथा वेदों का विशेष ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ भी करवा सकता है। आजकल कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। इससे व्यावसायिक गतिशीलता का पता चलता है।
(vii) भोजन प्रतिबंधों में कमी (Decline in Food Restrictions)-जातीय आधार पर भोजन संबंधी नियम काफी शिथिल हुए हैं। पढ़ी-लिखी नई पीढ़ियों में कच्चे तथा पक्के भोजन की अवधारणा खत्म होती जा रही है। होटलों, ढाबों, लंगरों, मंदिरों में किस जाति का व्यक्ति भोजन बांट रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है। होटल, क्लब में जाकर व्यक्ति यह नहीं पूछता है कि किस ने खाना बनाया या परोसा है। इस तरह भोजन प्रतिबंधों में काफी हद तक कमी आई है।
प्रश्न 5.
कबीला अथवा जनजाति क्या होती है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करो।
अथवा
जनजातीय समुदाय क्या है?
उत्तर:
हमारे देश में एक सभ्यता ऐसी होती है जो हमारी सभ्यता से दूर पहाड़ों, जंगलों, घाटियों इत्यादि में आदिम तथा प्राचीन अवस्था में रहती है। इस सभ्यता को कबीला, आदिवासी, जनजाति इत्यादि जैसे नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संविधान में इन्हें पट्टीदर जनजाति भी कहा गया है। कबाइली समाज वर्गहीन समाज होता है। इसमें किसी प्रकार का स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। प्राचीन समाजों में कबीले को बहुत ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह माना जाता था।
कबाइली समाज की अधिकतर जनसंख्या पहाड़ों अथवा जंगली इलाकों में पाई जाती है। यह लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। – यह समाज आमतौर पर स्वः निर्भर होते हैं जिनका अपने ऊपर नियंत्रण होता है तथा यह किसी के भी नियंत्रण से दूर होते हैं। कबाइली समाज शहरी समाजों तथा ग्रामीण समाजों की संरचना तथा संस्कृति से बिल्कुल ही अलग होते हैं। इनको हम तीन श्रेणियों में बांट देते हैं-शिकार करने वाले तथा मछली पकड़ने वाले और कंदमूल इकट्ठा करने वाले, स्थानांतरित तथा झूम कृषि करने वाले तथा स्थानीय रूप से कृषि करने वाले। यह लोग हमारी संस्कृति, सभ्यता तथा समाज से बिल्कुल ही अलग होते हैं।
जनजाति की परिभाषाएँ
(Definitions of Tribe)
(1) इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया (Imperial Gazetear of India) के अनुसार, “कबीला परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक नाम होता है, इसके सदस्य एक ही भाषा बोलते हैं तथा एक ही भू-भाग में रहते हैं तथा अधिकार रखते हैं अथवा अधिकार रखने का दावा करते हैं तथा जो अंतर्वैवाहिक हों चाहे अब न हों।”
(2) गिलिन तथा गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, “कबीला स्थानीय कुलों तथा वंशों की एक व्यवस्था है जो एक समान भू-भाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं तथा एक जैसी ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं।’
इस तरह इन अलग-अलग परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीले छोटे समाजों के रूप में एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। कबीले अपनी सामाजिक संरचना, भाषा, संस्कृति जैसे कई पक्षों के आधार पर एक दूसरे से अलग-अलग तथा स्वतंत्र होते हैं। हरेक जनजाति की अलग ही भाषा, संस्कृति, परंपराएं, खाने-पीने इत्यादि के ढंग होते हैं।
इनमें एकता की भावना होती है क्योंकि यह एक निश्चित भू-भाग में मिलजुल कर रहते हैं। यह बहुत से परिवारों का एकत्र समूह होता है जिस में काफ़ी पहले अंतर्विवाह भी होता था। आजकल इन कबाइली लोगों को भारत सरकार तथा संविधान ने सुरक्षा तथा विकास के लिए बहुत सी सुविधाएं जैसे कि आरक्षण इत्यादि दिए हैं तथा धीरे-धीरे यह लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं।
जनजाति की विशेषताएँ
(Characteristics of a Tribe)
1. परिवारों का समूह (Collection of Families)-जनजाति बहुत-से परिवारों का समूह होता है जिन में साझा उत्पादन होता है। वह जितना भी उत्पादन करते हैं उससे अपनी ज़रूरतें पूर्ण कर लेते हैं। वह कुछ भी इकट्ठा नहीं करते हैं जिस कारण उनमें संपत्ति की भावना नहीं होती है। इस कारण ही इन परिवारों में एकता बनी रहती है।
2. साझा भौगोलिक क्षेत्र (Common Territory) कबीलों में लोग एक साझे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण यह बाकी समाज से अलग होते हैं तथा रहते हैं। यह और समाज की पहुँच से बाहर होते हैं क्योंकि इन की अपनी ही अलग संस्कृति होती है तथा यह किसी बाहर वाले का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते इसलिए यह बाकी समाज से कोई रिश्ता नहीं रखते। इनका अपना अलग ही एक संसार होता है। इनमें सामुदायिक भावना पायी जाती है क्योंकि यह साझे भू-भाग में रहते हैं।
3. साझी भाषा तथा साझा नाम (Common Language and Common Name)-प्रत्येक कबीले की एक अलग ही भाषा होती है जिस कारण यह एक-दूसरे से अलग होते हैं। हमारे देश में कबीलों की संख्या के अनुसार ही उनकी भाषाएं पायी जाती हैं। हरेक जनजाति का अपना एक अलग नाम होता है तथा उस नाम से ही यह कबीला जाना जाता है।
4. खंडात्मक समाज (Segmentary Society)-प्रत्येक जनजातीय समाज दूसरे जनजातीय समाज से कई आधारों जैसे कि खाने-पीने के ढंगों, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि के आधार पर अलग होता है। यह कई आधारों पर अलग होने के कारण एक-दूसरे से अलग होते हैं तथा एक-दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं पाया जाता। इस कारण इनको खंडात्मक समूह भी कहते हैं।
5. साझी संस्कृति (Common Culture)-प्रत्येक जनजाति के रहन-सहन के ढंग, धर्म, भाषा, टैबु इत्यादि एक-दूसरे से अलग होते हैं। परंतु यह सभी एक ही कबीले में समान होते हैं। इस तरह सभी कुछ अलग होने के कारण एक ही कबीले के अंदर सभी कबीले के अंदर सभी व्यक्तियों की संस्कृति भी समान ही होती है।
6. आर्थिक संरचना (Economic Structure)-प्रत्येक जनजाति के पास अपनी ही भूमि होती है जिस पर वह अधिकतर स्थानांतरित कृषि ही करते हैं। वह केवल अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करना चाहते हैं जिस कारण उनका उत्पादन भी सीमित होता है। वह चीज़ों को एकत्र नहीं करते जिस कारण उनमें संपत्ति को एकत्र करने की भावना कारण ही जनजातीय समाज में वर्ग नहीं होते। प्रत्येक चीज़ पर सभी का समान अधिकार होता है तथा इन समाजों में कोई भी उच्च अथवा निम्न नहीं होता है।
7. आपसी सहयोग (Mutual Cooperation)-कबीले का प्रत्येक सदस्य कबीले के और सदस्यों को अप सहयोग देता है ताकि कबीले की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। कबीले में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा भी प्राप्त होती है। अगर कबीले के किसी सदस्य के साथ किसी अन्य कबीले के सदस्य लड़ाई करते हैं तो पहले कबीले के अन्य सदस्य अपने साथी से मिलकर दूसरे कबीले से संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रत्येक जनजाति के मुखिया का यह फर्ज होता है कि वह अपने कबीले का मान सम्मान रखे। कबीले के मुखिया के निर्णय को संपूर्ण कबीले द्वारा मानना ही पड़ता है तथा वह मुखिया के निर्णय की इज्जत भी इसी कारण ही करते हैं। कबीले के सभी सदस्य कबीले के प्रति वफ़ादार रहते हैं।
8. राजनीतिक संगठन (Political Organization)-कबीलों में गांव एक महत्त्वपूर्ण इकाई होता है तथा 10-12 गांव मिलकर एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं। यह बहुत सारे संगठन अपनी एक कौंसिल बना लेते हैं तथा प्रत्येक कौंसिल का एक मुखिया होता है। प्रत्येक कबाइली समाज इस कौंसिल के अंदर ही कार्य करता है। कौंसिल का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। कबीले का प्रत्येक सदस्य कबीले के प्रति वफ़ादार होता है।
9. कार्यों की भिन्नता (Division of Labour)-कबाइली समाज में बहुत ही सीमित श्रम-विभाजन तथा विशेषीकरण पाया जाता है। लोगों में भिन्नता के कई आधार होते हैं जैसे कि उम्र, लिंग, रिश्तेदारी इत्यादि। इनके अतिरिक्त कुछ कार्य अथवा भूमिकाएं विशेष भी होती हैं जैसे कि एक मुखिया तथा एक पुजारी होता है। साथ में एक वैद्य भी होता है जो बीमारी के समय दवा देने का कार्य भी करता है।
10. स्तरीकरण (Stratification)-कबाइली समाजों में वैसे तो स्तरीकरण होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो वह भी सीमित ही होता है क्योंकि इन समाजों में न तो कोई वर्ग होता है तथा न ही कोई जाति व्यवस्था होती है। केवल लिंग अथवा रिश्तेदारी के आधार पर ही थोड़ा-बहुत स्तरीकरण पाया जाता है।
प्रश्न 6.
भारत में मिलने वाले अलग-अलग कबीलों के राजनीतिक संगठनों का वर्णन करें।
उत्तर:
भारत में मिलने वाले कबीलों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं-
- उत्तर पूर्वी कबीले (North Eastern Tribes)
- मध्य भारतीय कबीले (Central Indian Tribes)
- दक्षिण भारतीय कबीले (South Indian Tribes)
अब हम इनका वर्णन विस्तार से करेंगे।
1. उत्तर पूर्वी कबीलों के राजनीतिक संगठन (Political Organization of North Eastern Tribes)-उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि जैसे प्रदेश ले सकते हैं। इन प्रदेशों के प्रमुख कबीले नागा, मिज़ो, अपातनी (Apatani), लुशाई, जंतिया, गारो, खासी इत्यादि आते हैं।
असम में मिलने वाले कबीलों में लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर कबीलों में भूमि के सामूहिक स्वामित्व को मान्यता प्राप्त है तथा साथ ही साथ भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों को भी मान्यता प्राप्त है। एक गांव के लोग कहीं पर भी कृषि करने को स्वतंत्र हैं। चाहे गांव के अलग-अलग परिवारों की आर्थिक स्थिति अलग होती है। परंतु इस अंतर से इनके समाज में कठोर सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न नहीं हुआ है। इनमें से अधिकतर कबीले बहिर्वैवाहिक गोत्रों में बंटे होते हैं, बाकी बचे कबीले गांव के समुदायों में गोत्र व्यवस्था के बिना रहते हैं। यह अलग अलग गोत्र अपने मुखिया के अंतर्गत कार्य करते हैं।
खासी कबीले में मुखिया की मृत्यु के बाद उसकी पदवी बड़ी बहन के बड़े पुत्र को प्राप्त होती है। अगर कोई आदमी मौजूद नहीं है तो बड़ी बहन की बड़ी बेटी को मुखिया बनाया जाता है। प्राचीन समय में खासी कबीला 25 खासी प्रदेशों में बँटा हुआ था जो कि एक-दूसरे से स्वतंत्र थे।
इन कबीलों में प्रशासन लोकतांत्रिक होता था जिसका कि एक मुखिया भी होता था। खासी कबीले में मुखिया न तो लोगों पर कोई कर लगा सकता था, न ही वह स्वतंत्र तौर पर कोई नीति बना सकता था तथा न ही उसको भूमि या जंगल से संबंधित कोई अधिकार था। जनता की राय के अनुसार निर्णय लिए जाते थे। निर्णय लेने के लिए कबीले के सभी बालिगों की सभा बुलाई जाती थी तथा लोगों को इसमें भाग लेना ही पड़ता था। लुशाई कबीले में चाहे मुखिया के पास अधिक अधिकार थे परंतु, यहां भी उसके लिए गांव के बुजुर्गों या सभा के निर्णय के विरुद्ध जाना मुमकिन नहीं था। चाहे मुखिया या और पद पैतृक थे परंतु प्रशासन लोकतांत्रिक होता था।
गारो कबीले में राजनीतिक प्रशासन लोकतान्त्रिक रूप से ही चलता था। गारो कबीले में कोई मुखिया (Chiefs) नहीं होते केवल एक Headman होता है जो कि कबीले का नाममात्र का मुखिया होता है। गांव या कबीले में सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय गांव की कौंसिल अथवा सभा द्वारा लिए जाते हैं जिसमें परिवारों के बुजुर्ग सदस्य होते हैं। नागा कबीले के राजनीतिक संगठन में बहुत अधिक विविधता (Diversity) देखने को मिल जाती है। कुछ नागा कबीले मुखिया की निरंकुश (Autocratic) मर्जी पर चलते हैं जबकि कुछ नागा कबीलों में लोकतांत्रिक गांव की सभा होती है जिस में Headman को बहुत ही कम अधिकार होते हैं।
अधिकतर नागा कबीलों को अत्याचारी, हिंसक, रक्त के प्यासे समझा जाता है परंतु इस तरह के विचार बनाना ठीक नहीं है। चाहे अधिकतर नागा कबीलों को लड़ाई के मैदान में देखा जा सकता है परंतु इस को सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए। बहुत-से लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि इस तरह की अव्यवस्था में स्थिर प्रशासन कैसे स्थापित हो सकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक कानून है। परंतु इन हालातों में भी लचकीले प्रकार का राजनीतिक संगठन देखने को मिल जाता है। कोनयाक (Konyak) कबीले में तो मुखिया को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागा कबीले में तो प्राकृतिक आपदाओं तथा प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए राजनीतिक संगठन तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं।
2. मध्य भारत के कबीले (Central Indian Tribes)-भारत में सबसे अधिक कबीले मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा के इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इन कबीलों में गोत्रों की एकता के आधार पर राजनीतिक संगठन के कुछ तत्त्व एक जैसे हैं। गांव के मुखिया की सहायता के लिए बुजुर्गों की एक सभा होती है जो गांव के प्रशासन की देख-रेख करती है। इस सभा में निर्णय या तो आम राय से लिए जाते हैं अथवा बहुमत से लिए जाते हैं तथा मुखिया के लिए सभा के निर्णय के विरुद्ध जाना मुश्किल नहीं होता है।
इस क्षेत्र के बहुसंख्यक कबीले भील, गौंड तथा ऊराओं लोग हैं। ऊराओं लोगों ने ‘Parha’ संगठन का निर्माण किया है जो कि बहुत-से पड़ोसी गांवों का संगठन होता है जिस में एक केंद्रीय संगठन ‘परहा पंच’ होता है। प्रत्येक ऊराओं परहा में कई गांव होते हैं। इनमें से एक गांव को रहा (राजा) गांव कहते हैं, दूसरे गांव को दीवान कहते हैं, तीसरे को पनरी (राजा का क्लर्क) कहते हैं, चौथे को कोतवाल गांव कहते हैं और सभी गांवों में से किसी को भी अधिक सत्ता प्राप्त नहीं है तथा उन्हें प्रजा कहा जाता है। राजा गांव को परहा का मुखिया गांव कहा जाता है। परहा के प्रत्येक गांव का अपना एक झंडा होता है तथा बैज (Badge) होता है जो किसी और गांव का नहीं होता है। परहा कौंसिल का मुख्य कार्य अलग अलग गांवों के बीच झगड़े निपटाना है।
संथाल लोगों में सब से निम्न राजनीतिक सत्ता गांव के मुखिया के पास होती है जिसे मंझी (Manjhi) कहा जाता है। मंझी तथा गांव के अन्य बुजुर्ग एक-दूसरे से मिलते हैं तथा गांव के मसलों के बारे में चर्चा करते हैं। मुखिया को विवाह के समय कुछ उपहार भी मिलते हैं तथा उसके पास बिना किराए की ज़मीन भी होती है। मंझी के पास सिविल तथा नैतिक सत्ता भी होती है। अपने दैनिक कार्यों के लिए उप-मुखिया उसकी मदद करता है।
मुंडा लोगों में गांव के मुखिया को मुंडा ही कहा जाता है परंतु धार्मिक मुखिया को ‘पहां’ (Pahan) कहा जाता है। 12 गांवों को मिला कर एक पट्टी अथवा परहा का निर्माण होता है जिसके मुखिया को ‘मनकी’ (Manki) कहा जाता है। गांवों के मुखिया एक समूह का निर्माण करते हैं जिनमें मनकी सबसे प्रभावशाली होता है। गौंड लोगों में मूल राजनीतिक इकाई गांव होता है। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मंडल कहा जाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी गांव के कार्य करने लोग बिहार के बस्तर जिले में पाए जाते हैं। चाहे बस्तर के हिंदू राजा की इन लोगों पर कोई प्रभुता नहीं होती है परंतु फिर भी उस को सभी गौंड समूहों का आध्यात्मिक मुखिया माना जाता है।
3. दक्षिण भारतीय कबीले (South Indian Tribes) यह कबाइली क्षेत्र एक तथ्य से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है तथा वह तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में तकनीकी तथा आर्थिक रूप से संसार के सबसे पिछड़े हुए कबीले रहते हैं। इस क्षेत्र के अधिकतर कबीले छोटे-छोटे समूह बना कर रहते हैं तथा वह या तो जंगलों में फैले (dispersed) हुए होते हैं या फिर गांवों के किसानों के पास कार्य करते हैं। आम तौर पर यह लोग अपने अनुसार ही जीवन जीते हैं तथा यह किसी बाहरी शक्ति के साथ संपर्क तथा हस्तक्षेप से दूर रहना ही पसंद करते हैं।
अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के कबीले अभी भी आर्थिक विकास की शिकारी तथा भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था में जी रहे हैं। इनमें से बहुत से घुमन्तू समूह होते हैं परंतु फिर भी यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही घूमते रहते हैं। प्रत्येक स्थानीय समूह में 5-10 परिवार होते हैं तथा हरेक समूह का अपना ही मुखिया होता है। यह स्थानीय समूह अलग ही रहते तथा कार्य करते हैं। चाहे विशेष शिकार करने के समय अथवा कुछ उत्सवों के समय यह अस्थायी तौर पर एक-दूसरे से मिल जाते हैं। इन स्थानीय समूहों के मुखिया ही इनके अंदरूनी मामलों की देख-रेख करते हैं।
कई और घुमंतु कबीलों में समूह के मुखिया नाम की कोई पदवी नहीं है। परिवारों के मुखिया इकट्ठे बैठते हैं तथा जब भी कोई समस्या सामने आती है तथा निर्णय लेने होते हैं तो वह सभी इकट्ठे होकर मसले का निपटारा करते हैं। अलार (Allar) तथा अरंडर (Arandar) लोगों में कोई मुखिया नहीं होता है। समूह के बुजुर्गों में एक जगह एकत्र होने के समय पर समुदाय के मसलों पर चर्चा होती है तथा इनका निर्णय सभी को मानना ही पड़ता है। जो लोग निर्णय को नहीं मानते हैं वह समूह को छोड़ कर चले जाते हैं तथा दूसरे समूह का हिस्सा बन जाते हैं। कदार (Kadar) लोगों में मुखिया की संस्था अब खत्म हो गई है।
केरल के अदियार (Adiyar) कबीले में मुखिया का पद पैतृक होता है। यदि पद के लिए पुत्र ठीक नहीं है तो भतीजे को पद प्राप्त हो जाता है। मुखिया एक विशेष पद है परंतु वह एक निरंकुश
(Autocratic) शासक नहीं होता है। वह केवल बुजुर्गों की मीटिंग की प्रधानता करता है जिसमें समुदाय के मामलों की चर्चा होती है।
प्रश्न 7.
जनजातीय विवाह क्या होता है? जनजातियों में जीवन साथी चुनने के कौन-कौन से तरीके हैं?
उत्तर:
भारत में जनजातीय विवाह (Tribal Marriage in India)-भारत में सैंकड़ों जनजातीय समूह निवास करते हैं। प्रत्येक जनजाति में अपनी अलग संस्कृति, रीति-रिवाज, विश्वास एवं धर्म होता है। अलग संस्कृति होने के कारण इनकी अलग पहचान भी होती है। भारत में कुछ जनजातियां त्योहारों या उत्सवों के अवसर पर विवाह पूर्व या विवाहेत्तर यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करती हैं। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इन समाजों में विवाह संबंधी कोई नियम ही नहीं है।
विवाह संबंधी अनेक नियम भी जनजाति की अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जनजातियों में आमतौर पर एक विवाह की प्रथा पाई जाती है। विभिन्न जनजातियों थेडा, अंडमानी, चेंचू, कादर इत्यादि सबसे कम विकसित जनजातियां हैं। जीवन साथी के चुनाव में भी जनजातीय समाजों में अनेक नियम व निषेधों की पालना की जाती है।
जनजाति में विवाह के प्रकार (Types of Marriage in Tribes) भारतवर्ष में भारतीय जनजातियों में पाए जाने वाले विवाह के प्रमुख स्वरूपों का वर्णन निम्नलिखित है:
1. एक विवाही प्रथा (Monogamy)-भारत की अधिकतर जनजातियों में एक विवाह की प्रथा का प्रचलन है। एक विवाह प्रथा के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक समय में केवल एक ही विवाह कर सकता है। भारतीय मुख्यः जनजातियों, जैसे संथाल, मुंडा, ओकाओ, हो, गोंड, भील, कोर्वा, जुआंगा, लीठा, बिरहोल, भोत, मिना, कादर, मीजो इत्यादि में एक विवाही प्रथा ही प्रचलित है।
2. बहु विवाह प्रथा (Polygamy) बहु विवाह प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति एक समय में एक से अधिक स्त्री/पुरुषों के साथ विवाह कर सकता है। भारत की अनेक जनजातियों में बहु विवाह प्रचलित है।
बहु विवाह दो प्रकार का है।
- बहु पति विवाह (Polyandry)
- बहु पत्नी विवाह Polygany)।
1. बहु पति विवाह (Polyandry)-बहु पति विवाह प्रथा के अंतर्गत एक स्त्री के एक समय में अनेक पति होते हैं अर्थात अनेक पति एक पत्नी। भारत की कई जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। भारत आर्य तथा मंगोल जनजातियों, थेडा, कोटा, खासा तिब्बत के लोगों में भी सामान्यतया इसी प्रथा का पालन होता है। बहु पति विवाह के भी आगे दो रूप हैं।
भ्रातृत्व बहु पति और अभ्रातृत्व बहु पति विवाह-भ्रातृत्व बहु पति विवाह में कई सगे भाइयों की एक ही समय में एक ही पत्नी होती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भ्रातृत्व बहुपति प्रथा पाई जाती है। अभ्रातृत्व बहुपति प्रथा के अंतर्गत अनेक पति आपस में सगे भाई नहीं होते। अनेक विभिन्न व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करते हैं तथा उनकी पत्नी थोड़े-थोड़े समय के लिए बारी-बारी सबके पास जाती है। टोडा, नापर, कोटा, मन्ना आदि जनजातियों में यही प्रथा प्रचलित है।
2. बह पत्नी विवाह (Polygany)-इस प्रथा के अंतर्गत एक समय में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। बहू पत्नी विवाह का यह रूप अनेक भारतीय जनजातियों में पाया जाता है। इन जनजातियों के समाज में इस प्रथा का पालन करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। नागा, गोंड, थेडा, लोशाई, पालियन, पुलामो इत्यादि जनजातियों में बहु पत्नी विवाह प्रथा ही पाई जाती है।
भारतीय जनजातियों में उपर्युक्त विवाह के स्वरूपों के अतिरिक्त कुछ विवाह अधिमानिक अर्थात् आदेशात्मक भी होते हैं। अधिमानक (Preferential) विवाहों के अंतर्गत चचेरे, ममेरे, भाई-बहनों का विवाह (Cross Cousin Marriage) नियोग एवं भगिनीयता (Levirate & Sorarate) विवाह आते हैं। चचेरे, ममेरे, भाई-बहिन किसी व्यक्ति के परिवार के दोनों ओर से भी हो सकते हैं अर्थात् पिता की बहन या माता के भाई या पिता के भाई के बच्चे भी हो सकते हैं।
ये विवाह अपने चाचा, मामा इत्यादि के बच्चों में किया जाता है। इस तरह नियोग तथा भगिनीयता विवाह भी इसी समाज में पाया जाता है। नियोग (Levirate) विवाह में एक व्यक्ति अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से विवाह कर सकता है। भगिनीयता विवाह में व्यक्ति का विवाह साली (Sister in Law) से किया जाता है। नियोग और भगिनीयता विवाह विशेष रूप से अंतर पारिवारिक दायित्वों की स्वीकृति पर बल देते हैं। इन प्रथाओं में विवाह के दो व्यक्तियों की अपेक्षा दो परिवारों के बीच संबंध को अधिक मान्यता दी जाती है।
जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके – (Tribal ways of Choosing & Life-Mate):
जनजातियों में विवाह यौन सुख, संतान उत्पत्ति व आपसी सहयोग के विकास के लिए किया जाता है। हिंदू समाज की तरह जनजातियों में विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता बल्कि इसमें विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में देखा जाता है। जनजातियों में मुख्यतः निम्न प्रकार के विवाह संबंध विकसित किये जाते हैं-
1. सह-पलायन विवाह (Elopment Marriage)-विवाह योग्य लड़का-लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं तथा विवाह कर लेते हैं। उसे सह-पलायन कहते हैं। इसके बाद बड़े-बूढ़े व्यक्ति इनकी जोड़ी को स्वीकार कर लेते हैं। यह विवाह पद्धति मुख्यतः वधू की ऊंची कीमत के कारण विकसित हुई मानी जाती है। सह-पलायन या घर से भाग कर विवाह का प्रचलन मुख्यतः किन्नौर, लाहौल स्पीति, छोटा नागपुर एवं झारखंड की जनजाति में है। झारखंड राज्य में ‘हो’ जनजाति में इस विवाह को राजी-खुशी विवाह कहा जाता है।
2. विनिमय विवाह (Marriage by Exchange)-इस प्रकार की विवाह प्रथा में दो परिवार स्त्रियों का आपस में आदान-प्रदान करते हैं। यह विवाह की विधि वधू की ऊंची कीमत के भुगतान से बचने के लिए विकसित की गई है। ये विवाह प्रथा संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में देखी जा सकती है। इस प्रथा के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी पत्नी प्राप्त करने के लिए उसके बदले में अपनी बहिन या परिवार की कोई स्त्री देता है। ये विधि खासी जनजाति की विशेषता है।
3. खरीद विवाह (Marriage by Purchase)-इस विवाह का रूप प्रारंभिक जनजातियों समाजों में अत्यधिक प्रचलित था। इस विवाह में वधू का मूल्य चुकाया जाता है। वधू के मूल्य का भुगतान नगद या फिर वस्तु के रूप में किया जाता है। मुख्य जनजातियां मुंडा, ओराओ, हो, संथाल, नागा, रेग्मां आदि में खरीद विवाह ही प्रचलित है। खरीद विवाह को क्रय विवाह भी कहा जाता है।
4. लूट विवाह (Marriage by Capture)-भारतीय जनजातियों में वधू प्राप्त करने का तरीका लूटकर विवाह करना है। यह प्रथा जनजातियों में वधू का अत्यधिक मूल्य का होने के कारण प्रचलित है। स्त्रियां लूटकर विवाह करने की प्रथा उत्तर:पूर्वीय क्षेत्र की नागा जनजातियों में अधिक प्रचलित है। इस प्रथा में एक जनजाति के लोग अपनी शत्रु जनजाति पर हमला करते हैं तथा लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। विवाह की ये प्रथा नागा, संथाल, मुंडा, गौंड, भील तथा पाई आदि जनजातियों में पायी जाती है।
5. सेवा विवाह (Marriage by Service)-इस विवाह प्रथा में लड़का अपने ससर के घर विवाह पूर्व एक निश्चित समय तक उसकी सेवा करता है। इस अवधि के पश्चात् यदि वधू का पिता उसकी सेवा से संतुष्ट होता है तो अपनी बेटी का हाथ उसे देता है। यदि वह उसके कार्य से असंतुष्ट होता है तो वर को घर से निकाल दिया जाता है। सेवा अवधि व सेवा स्वरूप भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। गौंड, बैगा आदि जनजातियों में ये प्रथा पाई जाती है।
6. हठ विवाह (Marriage by Intrusion) हठ विवाह के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ आत्मीयता के संबंध बनाता है। परंतु किसी न किसी बहाने से विवाह करने से हट जाता है तो वह स्त्री अपने-आप पहल करके उस व्यक्ति के घर में घुस जाती है। व्यक्ति के माता-पिता उसको मारते-पीटते हैं और प्रताड़ित करते हैं। यदि कन्या यह सह लेती है तो पड़ोस के लोग उस युवक को उस कन्या से विवाह के लिए बाध्य कर देते हैं। कई जनजातियों में इस विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है।
7. परीवीक्षा विवाह (Probationary Marriage)-इस विवाह के फलस्वरूप एक युवक निश्चित समय के लिए युवती के घर उसके पिता के साथ रहता है। इस परीवीक्षा काल में युवक व युवती यदि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है अन्यथा दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें क्षतिपूर्ति के रूप में युवक, युवती को कुछ दान देता है। इस परीवीक्षा अवधि में यदि युवती गर्भवती हो जाए तो युवक को उससे विवाह करना ही पड़ता है। मणिपुर की कूकी जनजाति में यह विवाह प्रथा प्रचलित है।
8. परीक्षा विवाह (Marriage by Test)-इस परीक्षा विवाह के अंतर्गत व्यक्ति तभी विवाह कर सकता है जब वह अपने आपको इसके लिए प्रमाणित कर लेता है। इस प्रथा में होली के अवसर पर सभी विवाह के इच्छुक नौजवान लड़के तथा लड़कियां एक पेड़ के नीचे या खंबे के पास इकट्ठे होकर (वृत्त बनाकर) नृत्य करते हैं। उस पेड़ या खंबे की चोटी पर नारियल और गुड़ बांधा जाता है। युवतियां पेड़ या खंबे के चारों ओर वृत्त बनाकर नृत्य करती हैं तथा युवक युवतियों के वृत्त के चारों और वृत्त बनाकर नाचते हैं।
हर युवक पेड़ या खंबे के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है। युवतियां इन्हें रोकने का पूरा प्रयास करती हैं। यहां तक कि युवक को रोकने के लिए उसे डंडे तक से भी पीटा जाता है। इस सबके बावजूद भी यदि युवक पेड़ या खंबे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और नारियल व गुड़ प्राप्त कर लेता है तो उसे नृत्य करती हुई किसी भी युवती के साथ विवाह करने की अनुमति मिल जाती है। उपर्युक्त स्वरूपों के आधार पर कहा जा सकता है कि अनेक जनजातियां अपने-अपने आधार पर विवाह के अनेक स्वरूपों को अपनाए हुए हैं।
प्रश्न 8.
परिवार का क्या अर्थ है? इसकी परिभाषाओं तथा विशेषताओं की व्याख्या करें।
उत्तर:
परिवार का अर्थ (Meaning of Family)-परिवार शब्द अंग्रेजी के शब्द ‘Family’ का हिंदी रूपांतर है। Family शब्द रोमन शब्द (Famulous) ‘फैमलयस’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘नौकर’ या ‘दास’.। इस तरह से रोमन कानून में परिवार से अभिप्राय है एक ऐसा समूह जिसमें नौकर या दास, मालिक या सदस्य शामिल हैं जो कि रक्त संबंधों के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित हों। इससे स्पष्ट है कि परिवार कुछ लोगों का इकट्ठा होना नहीं, बल्कि उनमें संबंधों की व्यवस्था है।
यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें औरत और आदमी का समाज से मान्यता प्राप्त लिंग संबंधों (Sex Relations) को स्थापित करता है। संक्षेप में, परिवार व्यक्तियों का वह समूह है, जो कि विशेष “नाम” से पहचाना जाता है जिसमें स्त्री एवं पुरुष का स्थायी लिंग संबंध हो, और इसी प्रक्रिया में सदस्यों के पालन-पोषण की व्यवस्था हो तथा उनमें रक्त के संबंध हों और वे एक विशेष निवास स्थान पर रहते हों।
परिवार ‘शब्द’ का सही अर्थ जानने के लिए यह आवश्यक है कि समाज शास्त्रियों की ओर से दी गई सभी परिभाषाओं को ठीक तरह से देख लें। इन सभी में थोड़ा-बहुत अन्तर तो है ही क्योंकि हर विद्वान् ने अपने दृष्टिकोण से और अपने-अपने हालातों के अनुसार परिभाषा दी है। इन सभी का वर्णन निम्न प्रकार से है-
(1) आगबर्न और निमकॉफ (Ogburn and Nimcoff) के अनुसार, “परिवार बच्चों सहित या बच्चों रहित, पति-पत्नी या अकेला एक आदमी या औरत और बच्चों की एक स्थाई सभा है।”
(2) मैकाइवर और पेज़ (Maclver and Page) के अनुसार, “परिवार एक ऐसा समूह है जो कि निश्चित एवं स्थायी लिंग संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों को पैदा करने एवं पालन-पोषण के अवसर प्रदान करता है।”
(3) मर्डोक (Mardock) के अनुसार, “परिवार एक ऐसा समूह है जिसकी विशेषताएं हमारा निवास स्थान, आर्थिक सहयोग और संतान की उत्पत्ति या प्रजनन हैं, इसमें दोनों लिंगों के बालिग शामिल होते हैं और इसमें कम से-कम दो के मध्य सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत लिंग संबंध होता है और लिंग संबंधों से बने इन बालिगों के अपने या गोद लिए हुए एक या इससे ज्यादा बच्चे होते हैं।” इस तरह उपरोक्त सभी समाज शास्त्रियों द्वारा दी गई परिवार की परिभाषाएं देखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है, जिसमें आदमी एवं औरत के लैंगिक संबंधों को समाज की तरफ से मान्यता प्राप्त होती है।
इस तरह से यह एक जैविक इकाई है जिसमें लैंगिक संबंधों की पूर्ति एवं संतुष्टि होती है और उससे बच्चे पैदा किए जाते हैं, बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है और उन्हें बड़ा किया जाता है। इस तरह यहां पर लिंग संबंधों को विधिपूर्वक स्वीकार किया जाता है और यह आर्थिक आधार पर भी टिका है। इसमें बच्चों की ज़िम्मेदारी भी शामिल है।
इस प्रकार परिवार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकता है। चाहे इसके अर्थों के बारे में अलग-अलग समाजशास्त्रियों के विचारों में भिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसमें मर्द तथा स्त्री के लैंगिक संबंधों को मान्यता प्रदान की जाती है तथा यह एक सर्वव्यापक समूह है जो प्रत्येक समाज में पाया जाता है। परिवार को एक जैविक इकाई के रूप में भी माना जा सकता है।
परिवार की विशेषताएँ
(Characteristics of Family)
1. परिवार एक सर्वव्यापक समूह है (Family is a universal group)-परिवार को एक सर्वव्यापक समूह माना जाता है क्योंकि यह प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक काल में पाया जाता रहा है। अगर इसे मनुष्यों के इतिहास के पहले समूह या संस्था के रूप में माने तो ग़लत नहीं होगा। व्यक्ति किसी-न-किसी परिवार में ही जन्म लेता है तथा वह तमाम उम्र उस परिवार का सदस्य बनकर ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य हमेशा ही होता है। इस कारण ही इसे सर्वव्यापक समूह माना जाता है। यहां तक कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी परिवार में ही होती है।
2. परिवार छोटे आकार का होता है (Family is of small size)-प्रत्येक परिवार छोटे तथा सीमित आकार का होता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति का जिस समूह अथवा परिवार में जन्म होता है उसमें या तो रक्त संबंधी या वैवाहिक संबंधी ही शामिल किए जाते हैं। प्राचीन समय में तो संयुक्त परिवार होते थे जिनमें बहुत से रिश्तेदार जैसे कि दादा-दादी, ताया-तायी, चाचा-चाची, उनके बच्चे इत्यादि शामिल होते थे। परंतु समय के साथ साथ बहत से कारणों के कारण समाज में परिवर्तन आए तथा संयुक्त परिवारों की जगह मूल परिवार सामने आए जिनमें केवल माता-पिता तथा उनके बिन विवाहित बच्चे रहते हैं। विवाह के बाद बच्चे अपना अलग मूल परिवार बना लेते हैं। इस प्रकार परिवार छोटे तथा सीमित आकार का होता है जिसमें रक्त संबंधी अथवा वैवाहिक संबंधी ही शामिल होते हैं।
3. परिवार का भावात्मक आधार होता है (Family has emotional base)-प्रत्येक परिवार का भावात्मक आधार होता है क्योंकि परिवार में रहकर ही व्यक्ति में बहुत-सी भावनाओं का विकास होता है। परिवार को समाज का आधार माना जाता है तथा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां परिवार पर ही निर्भर होती हैं। बहुत-सी भावनाएं तथा क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं जैसे कि पति-पत्नी के बीच संबंध, बच्चों का पैदा होना, वंश को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखना। परिवार में रहकर ही व्यक्ति में बहुत-सी भावनाओं का विकास होता है जैसे कि प्यार, सहयोग, हमदर्दी इत्यादि। इन सबके कारण ही परिवार समाज की प्रगति में अपना योगदान देता है।
4. परिवार का सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थान होता है (Family has a central position in Social Structure)-परिवार एक सर्वव्यापक समूह है तथा यह प्रत्येक समाज में पाया जाता है। इसे समाज का पहला समूह भी कहा जाता है जिस कारण समाज का संपूर्ण ढांचा ही परिवार पर निर्भर करता है। समाज में अलग-अलग सभाएं भी परिवार के कारण ही निर्मित होती हैं तथा इस वजह से ही परिवार को सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थान प्राप्त है।
प्राचीन समय में तो परिवार के ऊपर ही सामाजिक संगठन निर्भर करता था। व्यक्ति के लगभग सभी प्रकार के कार्य परिवार में ही पूर्ण हो जाया करते थे। चाहे आधुनिक समाज में बहुत-सी और संस्थाएं सामने आ गई हैं तथा परिवार के कार्य इन संस्थाओं द्वारा ले लिए गए हैं, परंतु फिर भी व्यक्ति से संबंधित बहुत से ऐसे कार्य हैं जो केवल परिवार ही कर सकता है और कोई संस्था नहीं कर सकती है।
5. परिवार का रचनात्मक प्रभाव होता है (Family has a formative influence)-परिवार नाम की संस्था ऐसी संस्था है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता है तथा इस कारण ही सामाजिक संरचना में परिवार को सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगर बच्चे का सर्वपक्षीय विकास करना है तो वह केवल परिवार में रहकर ही हो सकता है। परिवार में ही बच्चे को समाज में रहन-सहन, व्यवहार करने के ढंगों का पता चलता है।
बहुत से मनोवैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि शुरू के सालों में ही बच्चे ने जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। बाद की उम्र में तो उसमें केवल अच्छाई तथा बुराई जैसी चीजें ही विकसित होती हैं। बच्चा परिवार में जो कुछ होते हुए देखता है वह उसके अनुसार ही सीखता है तथा वैसा ही बन जाता है। इस प्रकार परिवार या व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता है।
6. यौन संबंधों को मान्यता (Sanction of Sexual relations)-व्यक्ति जब विवाह करता है तथा परिवार का निर्माण करता है तो ही उसके तथा उसकी पत्नी के लैंगिक अथवा यौन संबंधों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। परिवार के साथ ही मर्द तथा स्त्री एक-दूसरे से यौन संबंध स्थापित करते हैं। प्राचीन समाजों में यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई नियम नहीं थे तथा कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इस कारण ही परिवार का कोई भी रूप हमारे सामने नहीं आया था तथा समाज साधारणतया विघटित रहते थे। इस प्रकार परिवार के कारण ही मर्द तथा स्त्री के संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है।
प्रश्न 9.
परिवार के भिन्न-भिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।
अथवा
परिवार के विभिन्न प्रकारों या स्वरूपों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
यह संसार बहुत ही बड़ा है। इसमें कई प्रकार के समाज एवं सामाजिक इकाइयां पाई जाती हैं। हरेक समाज की अपनी उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। इसी कारण उन समाजों में अलग-अलग तरह के परिवार पाए जाते हैं। यह इस तरह होता है कि हर समाज के अलग-अलग रीति रिवाज, आदर्श विश्वास एवं संस्कृति होती है। एक ही देश, जैसे भारत में कई तरह के समाज पाए जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर, पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक समाज। इसी तरह से परिवारों के भी अनेक रूप हैं। इन्हीं रूपों को संख्या के आधार पर, विवाह के आधार पर, सत्ता के आधार पर एवं वंश के आधार पर तथा रहने के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। हम अभी इनको अलग-अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे।
1. विवाह के आधार पर परिवार की किस्म (On the basis of marriage)-
A. एक-विवाही परिवार (Monogamous Family)-इस तरह के परिवार में व्यक्ति एक ही औरत के साथ विवाह कर सकता है और उसी के साथ रहता हुआ सन्तान की उत्पत्ति करता है। आजकल इसी विवाह को आदर्श विवाह एवं ऐसे परिवार को सही परिवार माना जाता है।
B. बहु-विवाही परिवार (Polygamous Family)-इस तरह के परिवार में, जब एक आदमी एक से ज्यादा औरतों के साथ विवाह कर सकता है या फिर एक औरत, एक से ज्यादा पतियों से विवाह करती है तो इस प्रकार के विवाह को बहु-विवाही कहते हैं। यह भी आगे दो प्रकार का होता है-
(i) बहु-पति विवाह (Polyandrous Family)-जब कोई औरत एक से ज्यादा पतियों के साथ विवाह करवाती है, तो बहु-पति विवाह होता है। इस विवाह की विशेषता यह होती है कि एक औरत के कई पति होते हैं। इनमें यह भी दो प्रकार के होते हैं
- इसमें औरत के सभी पति सगे भाई होते हैं।
- दूसरी अवस्था में यह आवश्यक नहीं कि वे सभी सगे भाई हों।
(ii) बहु-पत्नी विवाह (Polygamous Family) इस प्रकार के विवाहों में, पति यानि कि आदमी एक से ज्यादा औरतों से विवाह करवाता है। इस प्रकार के परिवारों में एक आदमी की कई पत्नियां होती हैं। इस प्रकार के विवाह मुसलमानों में आमतौर पर मिल जाते हैं। इस तरह से मुस्लिम समुदाय में चार पलियां रखने की आज्ञा दी गई है। पुराने जमाने में हिंदू राजे-महाराजे भी कई पत्नियां रखते थे। सन् 1955 में हिंदू विवाह कानून के आधार पर हिंदुओं को एक से ज्यादा पत्नियां रखने का अधिकार नहीं है। परंतु भारत में अभी कई कबीलों में वही पुरानी परंपरा कायम है, जैसे नागा, गोण्ड, जिनमें इस तरह के परिवार अभी भी पाए जाते हैं।
2. सदस्यों के आधार पर परिवार की किस्में (Family on the basis of members)-सदस्यों के आधार पर परिवार के तीन प्रकार हैं-
A. केन्द्रीय परिवार (Nuclear Family)-यह एक छोटा परिवार होता है, जिसमें एक पति एवं पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इस परिवार में बाकी कोई भी रिश्तेदार या सदस्य नहीं होता। आजकल समाज में इन्हीं परिवारों की अधिकता है। इन परिवारों के सदस्य आमतौर पर शहरों में नौकरी करते हैं और जब उनके बच्चे विवाह करवा लेते हैं, तो वे भी एक केंद्रीय परिवार को जन्म दे देते हैं।
B. संयुक्त परिवार (Joint Family)-इस तरह के परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिसमें दादा-दादी, चाचा-चाची, भाई-भौजाई एवं ताया-तायी, उनके बच्चे, भाई-बहन आदि सभी इस प्रकार से शामिल होते हैं। इस प्रकार के परिवार अभी भी गाँवों में पाये जाते हैं।
C. विस्तृत परिवार (Extended Family) इस तरह के परिवार, संयुक्त परिवारों से ही बनते हैं। जब संयुक्त परिवार आगे बड़े हो जाते हैं, तो वे “विस्तृत परिवार’ कहलाते हैं। इनमें सभी भाई, उनके बच्चे विवाह के उपरांत भी साथ में रहते हैं चाहे उनके भी आगे बच्चे हो जायें। आजकल के समाजों में, इस तरह के परिवार मुमकिन नहीं हैं। प्राचीन काल में ऐसा हो जाता था, क्योंकि उनके काम-धंधे एक ही हुआ करते थे।
3. वंश नाम के आधार पर परिवार के प्रकार (On the basis of Nomenclature) इस आधार पर परिवार की चार तरह की किस्में मिलती हैं-
(i) पितृ-वंशी परिवार (Patrilineal Family) इस तरह का परिवार पिता के नाम से ही चलता है। इसका अर्थ ता का नाम उसके पुत्र को मिलता है और पिता के वंश का महत्त्व होता है। आजकल इस तरह के परिवार मिल जाते हैं।
(ii) मातृ-वंशी परिवार (Matrilineal Family)-इस तरह के परिवार माँ के नाम के साथ चलते हैं, जिसका अर्थ है कि बच्चे के नाम के साथ माता के वंश का नाम आएगा। माता के वंश का नाम बच्चों को प्राप्त होगा। इस प्रकार के परिवार भारत के कुछ कबीलों में भी मिल जाते हैं।
(iii) दो वंश नामी परिवार (Bilinear Family)-इस प्रकार के परिवारों में बच्चे को दोनों वंशों के नाम प्राप्त होते हैं और दोनों वंशों के नाम साथ-साथ में व्यक्ति के साथ चलते हैं।
(iv) अरेखकी परिवार (Non-Unilinear Family)-इस प्रकार के परिवारों में वंश के नाम का निर्धारण सभी नज़दीक के रिश्तेदारों के आधार पर होता है। इसको अरेखकी परिवार कहते हैं।
4. रिश्तेदारों के प्रकार के आधार पर परिवारों की किस्म (On the basis of types of Relatives)-इस प्रकार के परिवार भी दो प्रकार के होते हैं-
(i) रक्त संबंधी परिवार (Consanguine Family)-इस प्रकार के परिवारों में रक्त संबंधों का स्थान सबसे ऊपर होता है और इनमें किसी भी प्रकार के लिंग संबंध नहीं होते। इस परिवार में पति-पत्नी भी होते हैं, परंतु यह परिवार के आधार नहीं होते। इस परिवार में सदस्यता जन्म के आधार के कारण प्राप्त होती है। ये स्थायी होते हैं। तलाक भी इन परिवारों के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता।
(ii) विवाह संबंधियों का परिवार (Conjugal Family)-इस प्रकार के परिवारों में पति-पत्नी और उनके बिन ब्याहे बच्चे होते हैं अर्थात् जिनका विवाह अभी नहीं हुआ होता। इसमें पति-पत्नी और उनके रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। यह परिवार किसी की मौत के बाद या फिर तलाक के बाद भी भंग हो सकता है।
5. रहने के स्थान के आधार पर आधारित परिवार (Family on the basis of Residence)-इस प्रकार के परिवार तीन तरह के होते हैं-
(i) पितृ-स्थानी परिवार (Patrilocal Family)-इस प्रकार के विवाह के बाद, लड़की अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के घर रहने लग जाती है और इस तरह अपना परिवार बसाती है। इस तरह के परिवार आमतौर पर मिल जाते हैं।
(ii) मातृ-स्थानी परिवार (Matrilocal Family)-इस प्रकार के परिवार उपरोक्त परिवार से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनमें लड़की अपने पिता का घर छोड़कर नहीं जाती, वह उसी घर में ही रहती है। इसमें पति अपने पिता का घर छोड़कर, पत्नी के घर आकर रहने लग जाता है। इसको मातृ-स्थानी परिवार कहते हैं। ‘गारो’, खासी इत्यादि कबीलों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं।
(iii) नव-स्थानी-परिवार (Neo-Local-Family)-इस प्रकार के परिवार दोनों तरह की किस्मों से अलग हैं। इस तरह के विवाह के पश्चात् पति-पत्नी कोई भी एक-दूसरे के माता-पिता के घर नहीं जाते और न ही वहां रहते हैं। इसके विपरीत वे अपना और घर बनाते हैं और वहां पर जाकर रहते हैं। इस परिवार को नव-स्थानी परिवार कहा जाता है। आजकल के औद्योगीकरण के युग में बड़े-बड़े शहरों में, इस तरह के परिवार आम देखने में मिलते हैं।
6. सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार (On the basis of Authority)-इस तरह के परिवार भी दो तरह के होते हैं-
(i) पितृ सत्तात्मक परिवार (Patriarchal Family)-जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कि इस तरह के परिवार में शक्ति पिता के हाथों में होती है। परिवार के सभी कार्य पिता की मर्जी के अनुसार होते हैं। वह ही परिवार का कर्ता होता है। इस तरह से परिवार के सारे छोटे-बड़े कार्य का फैसला वह स्वयं ही करता है। भारत में इस तरह के परिवार ज्यादातर पाए जाते हैं।
(ii) मातृ-सत्तात्मक परिवार (Matriarchal Family)-इस तरह से यह भी नाम से ही प्रतीत होता कि इस तरह के परिवार में शक्ति माता के हाथ में होती है। मातृ सत्तात्मक परिवार में सभी फैसले एवं कर्ता माता होती है। बच्चों के ऊपर ज्यादा अधिकार माता का होता है। स्त्री ही इसमें मूल पूर्वज मानी जाती है। इसमें संपत्ति का वारिस माता का पुत्र नहीं होता, बल्कि उसका भाई अथवा ‘भांजा’ होता है। कई तरह के कबीलों जैसे गारो, खासी आदि में ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है।
प्रश्न 10.
एकाकी अथवा केंद्रीय परिवार का क्या अर्थ है? विशेषताओं सहित व्याख्या करें।
उत्तर:
केंद्रीय परिवार के अर्थ एवं परिभाषाएं-परिवार को संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रीय एवं संयुक्त परिवार। इसमें केंद्रीय परिवार छोटा परिवार माना जाता है, इसमें माता-पिता तथा उनके कुंवारे बच्चे ही रहते हैं। संयुक्त परिवार में दादा-दादी, माता-पिता, ताया-तायी और उनके सभी बच्चे साथ में ही रहते हैं। इस प्रकार से केंद्रीय परिवारों की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने तरीके से की है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-
(1) मर्डोक के अनुसार- केंद्रीय परिवार एक शादीशुदा आदमी और उसकी औरत और उनके बच्चों को मिलाकर बनता है, जबकि यह हो सकता है कि और व्यक्ति भी उनके साथ एक परिवार बना कहै।”
(2) इसी प्रकार से विदवान आर०पी० देसाई ने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है- ”केंद्रीय परिवार वह है, जिसके सदस्य, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ संपत्ति, आमदनी, अधिकार एवं कर्तव्यों द्वारा संबंधित न हों, जैसे कि रिश्तेदार से रिश्तेदारी की उम्मीद की जाती है।”
इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इकाई परिवार में केवल माता-पिता, उनके कुंवारे बच्चे ही रहते हैं और फिर जब उनका विवाह हो जाता है तो वे अपना अलग घर बना कर चले जाते हैं अर्थात् अपने अलग घर में रहते हैं। इस तरह से यह परिवार विवाह के आधार पर ही जुड़े होते हैं। इनका आकार भी छोटा ही होता है। इसमें नया जोड़ा अपना अलग घर बना कर रहता है। इसलिए इसको प्रजनन परिवार भी कहा गया है।
केंद्रीय अथवा इकाई परिवार की विशेषताएँ
(Characteristics of Nuclear Family)
1. छोटा आकार (Small Size)-इस तरह के परिवारों की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इनका आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसमें केवल माता-पिता और उनके कुंवारे बच्चे ही रहते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है, जैसे कि आजकल दो या तीन बच्चों का चलन है। इस तरह से जब यह बच्चे विवाह करते हैं तो यह अपने नए घर में जाकर रहते हैं।
2. सीमित संबंध (Limited Relations) केंद्रीय परिवार में ज़्यादा से ज्यादा आठ रिश्तों को माना गया है अथवा शामिल किया गया है, जैसे कि पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, पिता-पुत्री, माता-पुत्री, बहन-भाई, भाई भाई, बहन-बहन। इनमें द्वितीय रक्त के संबंधों का महत्त्व कम माना गया है। उन सदस्यों के साथ संबंध भी रस्मी तौर पर ही होते हैं। केंद्रीय परिवारों में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने परिवार द्वारा ही करता है।
3. प्रत्येक सदस्य का महत्त्व (Importance of every member) केंद्रीय परिवार में पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे ही रहते हैं तथा यह समानता पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के परिवार में दो पीढ़ियों के लोग ही रहते हैं तथा सभी को समान स्थिति ही प्राप्त होती है। पत्नी तथा बच्चों की स्थिति भी इसमें समान ही होती है। घर के सभी सदस्यों में कार्य बँटे हुए होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन-पोषण करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वह अपना भविष्य बना सकें। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को परिवार में समान महत्त्व प्राप्त होता है।
4. बराबर सत्ता (Common authority) संयुक्त परिवारों में घर की सत्ता परिवार के बड़े बुजुर्गों के हाथ में ही होती है तथा पत्नी और बच्चों का कोई महत्त्व नहीं होता है। परंतु केंद्रीय परिवार इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं जिनमें घर की सत्ता सभी के हाथ में समान रूप से होती है। घर में केवल पति या पिता की ही सत्ता नहीं चलती है बल्कि पत्नी तथा बच्चों की भी सत्ता चलती है।
घर की प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्या को हल करने के लिए उनकी सलाह ली जाती है। इसमें सभी की व्यक्तिगत योग्यता को महत्त्व प्राप्त होता है। यह परिवार परंपरागत परिवारों से अलग होते हैं तथा आधुनिक समाजों में चलते हैं।
5. वैवाहिक व्यवस्था (Marital System) केंद्रीय परिवार विवाह होने के बाद ही सामने आते हैं। अगर देखा जाए तो विवाह के बाद ही केंद्रीय परिवार निर्मित होते हैं। इस प्रकार के परिवार में पति-पत्नी तथा उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हैं। विवाह होने के बाद बच्चे अपना अलग घर बसाते हैं। प्राचीन समाजों में अधिक बच्चे हुआ करते थे परंतु आजकल के समय में केवल एक या दो बच्चे ही होते हैं। इस प्रकार के परिवार का आधार ही विवाह है तथा इस प्रकार के परिवार में बच्चे अपनी इच्छा से विवाह करवाते हैं।
6. व्यक्तिवादी दृष्टिकोण (Individualistic Outlook) संयुक्त परिवारों में परिवार के सभी सदस्य परिवार के हितों के लिए कार्य करते हैं तथा अपने हितों की तिलांजलि दे देते हैं। परंतु केंद्रीय परिवारों में ऐसा नहीं होता है। केंद्रीय परिवारों में लोग केवल अपने हितों को ही देखते हैं। उन्हें परिवार के हितों से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर परिवार पर कोई समस्या आती है तो यह घर छोड़ कर ही चले जाते हैं। उनका दृष्टिकोण सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिवादी होता है।
प्रश्न 11.
संयुक्त परिवार क्या होता है? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जहां पर 70% के करीब जनसंख्या कृषि अथवा उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर करती है। कृषि के कार्य में बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जिस कारण यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। यही प्रथा परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता भी है। ग्रामीण समाजों में गतिशीलता कम होती है जिस कारण भी लोग अपने घर छोड़ कर केंद्रीय परिवार बसाना पसंद नहीं करते।
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है संयुक्त परिवार में एक दो नहीं बल्कि तीन अथवा चार पीढ़ियों के लोग इकट्ठे मिल कर रहते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार में पड़दादा, पड़दादी, दादा-दादी, माता-पिता, ताया-तायी, चाचा-चाची तथा उनके बच्चे सभी शामिल होते हैं तथा इकठे मिल कर रहते हैं। संयुक्त परिवार में चाहे परिवार की संपत्ति घर के मुखिया के हाथों में होती है परंतु सभी का उस पर बराबर का अधिकार होता है।
परिभाषाएँ (Definitions) संयुक्त परिवार प्रणाली की सत्ता पिता के हाथ में होती थी। इस प्रणाली में पिता का कहना माना जाता था। इसमें पिता का कहना पत्थर के ऊपर लकीर वाला कार्य था। इसमें पिता की भूमिका एक निरंकुश शासक की तरह होती थी। इस प्रणाली में लड़के विवाह के पश्चात् भी उसी परिवार में ही रहते थे। अब भी अगर कई जगहों पर यदि संयुक्त प्रणाली है, तो उसमें विवाह के उपरांत सभी बच्चों को साथ में रहना होता है। इसी तरह उनकी आने वाली संतानें भी इकट्ठी रहती हैं।
(1) किंगस्ले डेविस (Kingslay Davis) के अनुसार, “संयुक्त परिवार में वे आदमी होते हैं, जिनके पूर्वज भी इकट्ठे हों, औरतों का विवाह न हुआ हो और अगर हुआ हो तो उनको समूह में शामिल किया जाए। ये सभी सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हों या इनके मकान एक-दूसरे के निकट होते हैं। किसी भी हालत में, जब तक संयुक्त परिवार इकट्ठा है, इसके सदस्य इसी के लिए मेहनत करते हैं और कुल संपत्ति का बराबर का हिस्सा प्राप्त करते हैं।”
(2) कार्वे (Karve) के अनुसार, “संयुक्त परिवार, उन आदमियों का समूह है, जोकि एक ही घर में रहते हैं और वे सभी एक ही रसोई में खाना बनाते हैं और वे सभी संयुक्त जायदाद के मालिक होते हैं। इस तरह वे सभी किसी न-किसी रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं।”
इस प्रकार इन परिभाषाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। यह सभी लोग एक साझे निवास स्थान पर रहते हैं तथा एक ही रसोई में पका हुआ भोजन खाते हैं।
संयुक्त परिवार में घर की सत्ता घर के मर्दो के हाथों में होती है जिस कारण घर की स्त्रियों की स्थिति भी निम्न होती है। घर की संपत्ति चाहे बड़े बुजुर्गों के हाथों में होती है परंतु सभी सदस्यों का इसमें समान अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य को उसके सामर्थ्य के अनुसार कार्य दिया जाता है तथा वह अपना कार्य अपना उत्तरदायित्व समझ कर पूर्ण करते हैं।
संयुक्त परिवार की विशेषताएँ
(Characteristics of Joint Family)
1. बड़ा आकार (Large in Size)-संयुक्त परिवार आकार में बहुत बड़ा होता है। इसमें माता-पिता के अतिरिक्त, उनके भाई-बहन, भाई, पुत्र, पुत्रियां एवं पौत्र इत्यादि सभी एक जगह इकट्ठे रहते हैं। इन सभी के अतिरिक्त इनके दादा-दादी भी मिलकर सभी के साथ रहते हैं। इस तरह से संयुक्त परिवार में कम-से-कम तीन पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में पिता के वंश से संबंधित कई पीढ़ियां इसमें रहती हैं। वे सभी मिलकर एक ही चारदीवारी के अंदर रहते हैं अर्थात् एक ही घर में रहते हैं। इस तरह से ये परिवार संख्या की दृष्टि से आकार में बड़े माने गए हैं।
2. संयुक्त संपत्ति (Joint or Common Property) संयुक्त परिवारों में सारी संपत्ति पर सभी का बराबर का अधिकार होता है। हर सदस्य इसमें अपनी योग्यता के आधार पर अपना योगदान डालता है। इसमें से जिस सदस्य को जितनी ज़रूरत होती है, वह खर्च कर लेता है। इस तरह परिवार का कर्ता जोकि प्रायः परिवार का बड़ा सदस्य होता है, सारी संपत्ति की देखभाल करता है। इस प्रकार से सारी संपत्ति के सभी. बराबर के मालिक होते हैं, परंतु परिवार का मुखिया इसको संभाल कर रखता है।
3. सहयोग की भावना (Feeling of Cooperation)-इस तरह के परिवारों में, सभी सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें कोई सदस्य ज्यादा काम करता है या कोई सदस्य कम कार्य करता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता। ऐसे परिवारों के सभी सदस्य एक निश्चित लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और वही उद्देश्य ही उन परिवारों के अस्तित्व को बचा कर रखता है।
4. संयुक्त रसोई (Common Kitchen)-संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी का खाना एक ही रसोई में तैयार होता है और सभी मिल-जुल कर उसे बनाते हैं। इस प्रक्रिया में इकट्ठे मिल-जुल कर खाते हैं और अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, ताकि उनका आपसी प्यार बना रहे।
5. संयुक्त निवास स्थान (Common Residence) संयुक्त परिवार की विशेषताओं में यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि उसके सभी सदस्य एक ही जगह पर अर्थात् एक ही मकान में रहते हैं। अगर उनकी रिहाइश को अलग-अलग कर दिया जाए, तो वह संयुक्त परिवार न होकर केंद्रीय परिवार हो जाएगा।
6. सदस्यों की सुरक्षा (Security of all Members) संयुक्त परिवार की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि यह परिवार अपने सभी सदस्यों की हर तरह से सुरक्षा करते हैं। इन परिवारों में उन सभी का संपत्ति पर अधिकार होता है। यदि कोई सदस्य बीमार हो जाये या उसके साथ कोई सुख-दुःख हो, परिवार के सभी सदस्य, उसकी देखभाल करते हैं।
उसके दुःख अथवा बीमारी पर जो भी खर्च आए, परिवार उसको सहन करता है। यदि किसी मर्द की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसकी पत्नी की ज़िम्मेदारी पूरा परिवार मिलकर संभालता है। उसके बच्चों की देख-रेख भी यही परिवार करता है। इस तरह से इस तरह के परिवारों के सभी सदस्य, उनकी संतानें अथवा स्त्रियां पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं।
7. संस्कृति की निरंतरता (Continuity of Culture) संयुक्त परिवार का यह मख्य लक्षण है कि उसका कर्ता या परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों पर पूरा अधिकार रखता है और इन परिवारों में पीढ़ियों से इकट्ठे रह रहे होते हैं और अगर यह परंपरा चलती रहे तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऐसा ही रहता है और उनके प्रेम प्यार में कोई कमी नहीं आती। यदि पिता ने अपने संस्कार पुत्र को दे दिए, वही आगे पुत्र ने अपने पुत्र को दे दिए, इस तरह से उनकी सभ्यता की धरोहर अर्थात् संस्कृति पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक चलती रहती है और उसकी निरंतरता बरकरार रहती है।
8. श्रम विभाजन (Division of Labour)-संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के कामों को बांट दिया जाता है। जिसको जो कार्य सौंप दिया जाता है, वह उसे अपना धर्म समझ कर निभाता है। कोई भी सदस्य अपनी मर्जी के अनुसार कार्य को बदल नहीं सकता। औरतें आमतौर पर घर पर रहकर, घर के काम करती हैं और घर के मर्द, बाहर जाकर रोटी-रोज़ी की समस्या का हल करते हैं अर्थात् कमाने की ज़िम्मेदारी आदमियों के ऊपर होती है।
इन परिवारों में कर्ता के स्थान को सबसे ऊपर माना गया है। इसके पश्चात् उसकी पत्नी का दूसरा नंबर होता है अर्थात् स्त्रियों में सबसे ज्यादा आदर कर्ता की पत्नी का होता है। इन परिवारों में विधवा स्त्री को ज़्यादा महत्त्व नहीं दिया जाता। इस तरह से सदस्यों की स्थिति भी उनके कार्य के अनुसार देखी जाती है। उसे उसकी स्थिति के अनुसार ही काम दिया जाता है।
9. संयुक्त परिवार में कर्ता की भूमिका (Role of Karta in Joint Family)-संयुक्त परिवार में कर्ता की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण होती है। इसमें प्रायः परिवार का सबसे ज़्यादा आयु का व्यक्ति अर्थात् कोई बुजुर्ग ही उसका कर्ता होता है। परिवार के सभी महत्त्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार उसे ही होता है और उसी तरह ही वह फैसला लेता भी है।
सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात कि वह उस परिवार की संपत्ति की चाहे वह चल हो या अचल, उसकी देखभाल उसे ही करनी पड़ती है। इन सारे कार्यों में बाकी परिवार के सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इन परिवारों में यदि कर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार का बड़ा लड़का फिर देखभाल करता है।

प्रश्न 12.
संयुक्त परिवार में लाभों तथा हानियों का वर्णन करें।
उत्तर:
संयुक्त परिवार के लाभ
(Merits of Joint Family)
1. सांस्कृतिक सुरक्षा (Cultural Security)-संयुक्त परिवारों के लाभों को देखने के लिए सबसे पहला पक्ष जो हमें नज़र आता है वह है उसका सामाजिक पक्ष। उसमें हम देख सकते हैं कि ये परिवार हमें सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों की देखभाल एवं पालन-पोषण मिल कर करते हैं।
इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यह परिवार हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रखते हैं; जैसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने से बड़ों का सम्मान करना, सभी के साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना और अपने कार्यों को अपना धर्म समझ कर पूरा करना। क्योंकि जो तीन पीढ़ियों के सदस्य इसमें रहते हैं, उनमें एक-दूसरे से मिलकर रहने की भावना रहती है। यह सभी तो इसकी संस्कृति होती है और यह व्यवस्था इसको स्थायी रूप से संभाल कर रखती है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित करती चली जाती है।
2. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)-संयुक्त प्रणाली अपने सदस्यों की, दुर्घटना, बीमारी एवं बेरोज़गारी अथवा अचानक किसी की मृत्यु हो जाये तो उन हालातों में रक्षा करती है अर्थात् देखभाल करती है। इस प्रकार यह अपने सदस्यों के लिए एक प्रकार की ‘बीमा कंपनी’ जैसा कार्य करती है। यह परिवार अपने बूढ़ों अथवा विधवा औरतों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
इन परिवारों में बच्चों की देखभाल भी अपने से बड़े सदस्यों द्वारा अपना समझ कर होती है। यदि कोई सदस्य मानसिक एवं शारीरिक तौर पर किसी भी पक्ष से कमज़ोर है, ये सदस्य उनकी देखभाल एवं रक्षा मिलजुल कर करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होने देते। उन्हें भी बराबरी का दर्जा एवं संपत्ति में बराबरी का अधिकार होता है।
3. बच्चों का पालन-पोषण (Taking Care of Children) संयुक्त परिवार में बच्चों के विकास की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है। इन परिवारों में बच्चों में नैतिक नियमों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। इन परिवारों में रहते हुए उदारता, सहयोग, प्यार, बड़ों की आज्ञा मानना एवं समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने की कला, तो इन परिवारों का प्रमुख लक्षण है।
इन गुणों में सबसे प्रमुख है, दूसरों के लिए जीने की कला, जो इन परिवारों में सबसे पहले सीखने को मिलती है। संयुक्त परिवार में सभी बच्चों के ऊपर नियंत्रण भी, उनको अनुशासन में रहने की आदत डालनी होती है। इसी तरह ही यह परिवार अपने बच्चों का पालन-पोषण करता है और परिवार का हर सदस्य उसमें बराबर की रुचि लेता है।
4. सामाजिक नियंत्रण (Social Control)-बगैर किसी ज़बरदस्ती के इस परिवार के सदस्यों को नियंत्रण में रहने की आदत पड़ जाती है। वे सभी स्वयं ही इस नियंत्रण को मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इसमें सभी की भलाई नज़र आती है। सदस्यों के आपसी संबंध एवं स्नेह प्यार के सामने यह नियंत्रण गौण नज़र आता है।
संयुक्त परिवार में कर्ता को सभी अधिकार दिए गए हैं, और वही अपने इस अधिकार को अपने परिवार की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करता है। यदि कोई सदस्य कोई ग़लत काम करता है तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर उसे डांट-फटकार भी सकता है। परंतु कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस तरह से यह परिवार अपने सदस्यों की सभी सामाजिक क्रियाओं पर पैनी नज़र रखते हैं और यही नियंत्रण ही उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है।
5. मनोरंजन का केंद्र (Centre of Recreation) संयुक्त परिवार अपने सभी सदस्यों को सही दिशा प्रदान करते हुए हर सुखद मौके का इंतज़ार करते रहते हैं। त्योहार इत्यादि, विवाह शादी का अवसर हो अथवा कोई धार्मिक कार्य या कोई और कोई भी सुखद मौका, उसे सभी सदस्य मिलजुल कर, हंसी-खेल करते हुए मनाते हैं।
बच्चे-बूढ़े, जवान और स्त्रियां इन्हीं अवसरों पर खूब मनोरंजन करते हैं और लोक गीतों, कहावतों, गानों और खेलों का आनंद मिलजुल कर लेते हैं और इन्हीं खेलों अथवा बातों-बातों में कई बार अपने तजुर्षों की बातें भी बच्चों को सिखा देते हैं। इस तरह से वे अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं।
6. चिंताओं से मुक्ति (Least Tensions of Life)-संयुक्त परिवार में बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। यदि कोई समस्या आ भी जाए, तो उसे सभी मिलजुल कर सुलझाते हैं। इन परिवारों में जो सहयोग की भावना होती है, उसका यही लाभ होता है कि सदस्यों के दिमाग पर कोई बोझ नहीं पड़ता और सभी आराम से खुशी-खुशी जीवन को जीते हैं।
संयुक्त परिवार की हानियाँ
(Demerits of Joint Family)
1. व्यक्तित्व के विकास में कमी (Lack of Personality Development) संयुक्त परिवार प्रणाली में यह कमी है कि इसमें व्यक्ति की अपनी योग्यता सही रूप में उभर कर सामने नहीं आ पाती क्योंकि उनके कार्यों का विभाजन इस तरीके से हो जाता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता।
व्यक्ति को अपने बड़ों के कहने पर अर्थात् कर्ता की इच्छानुसार कार्य करना होता है, वह सदस्य अपनी इच्छानुसार अपने बच्चों एवं पत्नी के साथ स्वतंत्रता के साथ समय नहीं बिता पाता। वह कई बार चाहते हुए भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, वह कोई भी कार्य अपने बड़ों की पसंद के बगैर नहीं कर सकता। इस प्रणाली में यह बहुत कमी है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सही तरह से दिखा नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर पारिवारिक नियंत्रण होते हैं।
2. औरतों की निम्न दशा (Low Status of Women) संयुक्त परिवार आमतौर पर पित-प्रधान होता है, अर्थात् इन परिवारों में पुरुषों का ज्यादा दबदबा होता है। इन परिवारों में पुरुषों की बात को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है, औरतों को परिवारों में ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते। उनकी ज़िम्मेदारी केवल रसोई और बच्चों की देखभाल की है।
संयुक्त परिवार में औरत की हैसियत सिर्फ बच्चों को पैदा करना और घर की चारदीवारी के अंदर ज़िन्दगी को जीना मात्र होता है। इस तरह की व्यवस्था में हमेशा आदमी और औरतों में तकरार अथवा लड़ाई-झगड़ा रहता है। इन परिवारों में औरत आर्थिक तौर पर पुरुष के ऊपर निर्भर होती है, इसलिए उनकी सामाजिक स्थिति दयनीय ही होती है।
3. खालीपन की प्रवृत्ति (Carelessness) संयुक्त परिवार प्रणाली में यह सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है आदमी में निकम्मापन आ जाता है अर्थात् उनको रोजी-रोटी की कोई समस्या तो होती नहीं, इस कारण उनमें खाली रहने अथवा आलस्य की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है और वह काम ही नहीं करना चाहते। इस समस्या के होते हुए कुछ सदस्यों को उन खाली सदस्यों का भी बोझ उन्हें ही उठाना पड़ता है और उनका काफ़ी समय उनको समझाने बुझाने एवं उनके हिस्से के कार्यों को करने में जाता है। इस तरह से ये प्रणाली व्यक्ति के निकम्मेपन को एक तरह से बढ़ाती है।
4. संघर्षपूर्ण स्थिति (Conflicts) संयुक्त परिवारों में आपसी लड़ाई-झगड़े बहुत होते हैं। इन परिवारों में कई बार एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। इस बात की चरम सीमा इतनी हो जाती है कि वह अपने भाई को मारने में भी संकोच नहीं करता। इस तरह से घर की शांति नष्ट हो जाती है।
इन परिवारों में कई बार स्त्रियों के कारण तनाव की स्थिति बन जाती है। कई बार ननद और भाभी की नहीं बनती। किसी जगह सास और बहु में क्लेश रहता है। कई बार व्यक्ति समझता है कि उसे अपनी योग्यता के अनुसार कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आपसी संघर्ष अपने आप जगह बना लेता है और कई बार ऐसी स्थितियों के कारण पूरा परिवार नष्ट हो जाता है।
5. ज़्यादा संतानोत्पत्ति (More Children)-संयुक्त परिवारों में क्योंकि सभी बच्चों के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी होती है कि कोई भी आदमी इस बात के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता कि उसको कितने बच्चों को पैदा करना है। संयुक्त परिवार में उनकी शिक्षा एवं पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी सभी की होने के कारण से कोई भी परिवार नियोजन की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं या कम बच्चे होते हैं, उन सभी की तरह होने के कारण, और यदि किसी के बच्चे कम होंगे और उसे कोई सीधा लाभ मिलेगा, इस कारण सभी ज़्यादा बच्चों को जन्म देते जाते हैं।
6. ग़रीबी को जन्म (Leads to Poverty) हर रोज की कलह-क्लेश, औरतों की निम्न स्थिति, निरंकुश विचारधारा का समाज, कर्तव्यों की तरफ विमुखता और ज़्यादा संतान की उत्पत्ति; यह सभी कारण, परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं और फिर समय के साथ-साथ इन परिवारों में अपनी नैतिक जिम्मेदारी को न समझना, यह सब परिवार को गरीब बना देता है।
परिवार का बढ़ते जाना और जमीन का न बढना और संपत्ति का स्थिर रहना, गरीबी का कारण बन जाता है। इसमें संपत्ति क्योंकि सभी की इकट्ठी होती है, उसकी सही ढंग से कोई भी देखभाल नहीं करता, इस कारण से बाद में उन्हें ही बदहाली झेलनी पड़ती है।
7. अन्य मिश्रित समस्याएँ (Other Mixed Problems)-उपरोक्त समस्याओं के अलावा कई मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी समस्याएं, मुकद्दमेबाजी इत्यादि, किसी को उसकी योग्यताओं अथवा क्षमताओं के आधार पर अधिकार न मिलना, यह सभी वस्तुएं. या कारण, आदमी को मनोवैज्ञानिक आधार पर तोड़ देती है।
प्रश्न 13.
संयुक्त परिवारों के विघटित होने के क्या कारण हैं? व्याख्या करें।
अथवा
क्या आपके विचार में संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है? व्याख्या करें।
अथवा
संयुक्त परिवार में परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए।
अथवा
क्या संयुक्त परिवार परिवर्तित/विघटित हो रहे हैं? स्पष्ट करें।
उत्तर:
इस प्रश्न का उत्तर हां में ही है। जी हां, आजकल हमारे विचार से संयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है। ये टूटने का जो सिलसिला है, एक-दो वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि यह बदलाव कई वर्षों के परिवर्तन का परिणाम है। यह सभी परिवर्तन कई भिन्न-भिन्न कारणों से आए, जिसके परिणामस्वरूप परिवारों की बनावट और उसके रूप में अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनको हम विस्तारपूर्वक इस संदर्भ में देखेंगे-
1. पैसों का महत्त्व (Importance of Money)-आधुनिक समाज में व्यक्ति ने पैसा कमाकर अपनी जीवन शैली में कई तरह के परिवर्तन ला दिए हैं और इस शैली को कायम रखने के लिए उसे हमेशा ज्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया में वह अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कमाई में बढ़ौतरी करने की कोशिश में लगा रहता है। उसके रहने-सहने का तरीका बदलता जा रहा है और ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं आज उसके जीवन के लिए सामान्य और आवश्यकता की वस्तुएं बनती जा रही हैं और इन सभी को पूरा करने के लिए पैसा अति आवश्यक है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि वह उन सीमित साधनों से ज़्यादा सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इस कारण संयुक्त परिवारों का महत्त्व कम हो रहा है और आदमी अपने परिवारों से अलग रहना पसंद करता है। यह उसकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी, इस कारण वह अपने परिवारों से अलग रहने लग गया है।
2. पश्चिमी प्रभाव (Impact of Westernization)-भारत में अंग्रेजों के शासनकाल और उसके बाद भारतीय समाज में कई तरह से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, जिससे कि हमारी संस्कृति और व्यवहार इत्यादि में कई जिनके कारण व्यक्तिवाद का जन्म होने लगा। आधनिक शिक्षा प्रणाली ने लोगों के जीवन को से रहने के तरीके सिखाए।
इस तरह से भौतिकतावादी सोच के कारण, आधनिकता की चकाचौंध से लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन शुरू हो गया और लोगों में संयुक्त परिवार से लगाव कम होना शुरू हो गया। इसका अंत में परिणाम यह निकला कि संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने लगी और इकाई अथवा केंद्रीय परिवार का उद्भव शुरू हो गया। लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली और औरतों की स्वतंत्रता के कारण, नौकरी करने वालों का शहरों में पलायन ने संयुक्त परिवारों का अस्तित्व समाप्त करना शुरू कर दिया और टूटना दिन-प्रतिदिन जारी है।
3. औद्योगीकरण (Industrialization) आधुनिक समाज को आज औद्योगिक समाज की संज्ञा दी जाती है। जगह-जगह पर कारखानों और नये-नये तरीकों से समाज में तबदीलियां नज़र आती हैं। हर रोज़ नये-नये आविष्कारों के कारण समाज में कार्य करने के तरीकों एवं मशीनीकरण का चलन बढ़ता जा रहा है। घरों में कार्य करने वाले लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। लोग अब अपने पैतृक कार्यों को छोड़कर उद्योगों में जा रहे हैं।
लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि इस दौड़ में अगर रहना है तो मशीनों का सहारा लेना ही पड़ेगा और इस बदलाव के कारण, शहरीकरण और भौगोलिक दृष्टि से कारखानों का बढ़ना इत्यादि लोगों को पलायन करवाता है। इस कारण लोगों ने संयुक्त परिवारों को छोड़कर, जहां पर उन्हें रोटी-रोज़ी मिली, वे उधर चल पड़े और यह सभी कुछ हुआ, उद्योगों के लगने की वजह से। इस तरह औद्योगीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि इकाई परिवारों का चलन या अस्तित्व, उद्योगों की वजह से बढ़ रहा है।
4. सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) आधनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति. उसकी योग्यता के आधार पर आंकी जाती है। इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा धन कमाना पड़ता है। हर व्यक्ति समाज में ऊपर उठना चाहता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति की स्थिति उसकी योग्यता के आधार पर न होकर अपने परिवार की हैसियत के अनुसार आंकी जाती है। इस प्रकार वह परिश्रम ही नहीं करता। औद्योगीकरण और शिक्षा के प्रसार ने व्यक्ति को गतिशील कर दिया है।
यातायात के साधनों और संचार के माध्यम से आदमी के लिए दूरियां कम हो गई हैं। उसका सोचने का तरीका बदलता जा रहा है। इस नए समाज में उसके जिंदगी के मूल्य भी बदल गए और वह भौतिकवाद की ओर अग्रसर है और उसी प्रक्रिया में उसमें भी तेजी आनी स्वाभाविक है और इस कारण वह संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है। इसी कारण से भी संयुक्त परिवारों का टूटना निरंतर जारी है।
5. यातायात के साधनों का विकास (Development of means of Communication and Transport) यहीं पर बस नहीं आधुनिक यातायात के साधनों में आया बदलाव भी अपने आप में इस सोच का कारण बना है। व्यक्ति को इन्हीं सुविधाओं के कारण ही नई राहों पर चलना आसान हो गया है। हर क्षेत्र में काम करने की संभावनाओं को इन्हीं साधनों ने बढ़ा दिया है, आज कोई भी व्यक्ति पचास-सौ किलोमीटर को कुछ भी नहीं समझता।
प्राचीन काल में यह सुविधाएं नहीं थीं या बहुत ही कम थीं, इस कारण से लोग एक ही जगह पर रहना पसंद करते थे। आज के युग में इन साधनों ने व्यक्ति की दूरियों को कम कर दिया है। इनकी वजह से भी आदमी बाहर अपने काम-धंधों को आसानी से कर पाता है और संयुक्त परिवार का मोह छोड़कर केंद्रीय परिवार की सभ्यता को अपना रहा है।
6. जनसंख्या में बढ़ोत्तरी (Increase in Population)-भारत में जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे कुछ ही समय में ही प्रत्येक परिवार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार की भूमि या जायदाद सारे सदस्यों के पालन पोषण के लिए काफ़ी नहीं होती और नौकरी या व्यवसाय की खोज में सदस्यों को परिवार छोड़ना पड़ता है। इसलिए भी संयुक्त परिवारों में विघटन हो रहा है।
7. शहरीकरण और आवास की समस्या (Problem of Urbanization and Immigration) संयुक्त परिवारों के टूटने का एक और महत्त्वपूर्ण कारण देश का तेजी से बढ़ता शहरीकरण है, जिससे लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। जबकि शहरों में मकानों की भारी कमी है। शहरों में मकान कम ही नहीं छोटे भी होते हैं। इसलिए मकानों की समस्या के कारण ही शहरों में संयुक्त परिवारों में विघटन हो रहा है।
8. स्वतंत्रता और समानता के आदर्श (Ideals of Independence and Equality) संयुक्त परिवार एक तरह से तानाशाही राजतंत्र है जिसमें परिवार के मुखिया का निर्देश शामिल होता है। इसका कहना सबको मानना पड़ता है व कोई उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता। इसलिए यह आधुनिक विचारधारा के विरुद्ध है। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से नए नौजवान लड़के और लड़कियों में समानता और स्वतंत्रता की भावना से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं।
प्रश्न 14.
परिवार की संस्था में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं? उनका वर्णन करें।
अथवा
परिवार के ढांचे तथा कार्यों में आ रहे परिवर्तनों का वर्णन करें।
अथवा
परिवार की संरचना के बदलते आयाम की व्याख्या कीजिए।
अथवा
संयुक्त परिवार में प्रमुख परिवर्तन क्या-क्या हुए हैं?
अथवा
परिवार में हुए किन्हीं दो परिवर्तनों का वर्णन करें।
अथवा
परिवार का अर्थ बताते हुए परिवार की संरचना में हुए नवीन परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उसके उत्पन्न होने से लेकर खत्म होने तक कोई परिवर्तन न आया हो। इस प्रकार समाज में सामाजिक संस्थाएं भी, जो हमारी सहायता के लिए बनाई गई थीं, इन सामाजिक संस्थाओं में भी समय के साथ-साथ परिवर्तन आ रहे हैं। इसी प्रकार परिवार नाम की संस्था शरू हई थीं उस समय से लेकर आज तक इसमें बहत परिवर्तन आ चके हैं।
उसके ढांचे के साथ-साथ कार्यों में भी बहुत से परिवर्तन आए हैं। ढांचा पक्ष से पहले संयुक्त परिवार होते थे अब वह केंद्रीय परिवारों में बदल रहे हैं। कार्यात्मक पक्ष से भी बहुत परिवर्तन आए हैं तथा इसके बहुत से कार्य और संस्थाओं के पास चले गए हैं। परिवार में आए परिवर्तनों का वर्णन इस प्रकार है-
1. केंद्रीय परिवारों का बढ़ना (Increasing Nuclear Families)-भारतीय समाज का एक परंपरागत ग्रामीण समाज है जहां पर प्राचीन समय में संयुक्त परिवार पाए जाते थे। मुख्य पेशा कृषि होने के कारण परिवार में अधिक सदस्यों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए संयुक्त परिवार हमारे समाज में पाए जाते थे। परंतु समय के साथ-साथ शिक्षा के बढ़ने से तथा सामाजिक गतिशीलता के बढ़ने से लोग शहरों की तरफ जाने लगे। लोग संयुक्त परिवारों को छोड़कर शहरों में जाकर केंद्रीय परिवार बसाने लगे। इस प्रकार परिवार के ढांचे पक्ष में परिवर्तन आने लग गए तथा संयुक्त परिवारों की जगह केंद्रीय परिवार सामने आने लग गए।
2. आर्थिक कार्यों में परिवर्तन (Change in Economic Functions)-परिवार के आर्थिक कार्यों में भी बहुत से परिवर्तन आए हैं। प्राचीन समय में तो व्यक्ति की आर्थिक क्रियाएं परिवार के इर्द-गिर्द ही सिमट कर रहती थीं। कार्य परिवार दवारा ही होता था तथा रोटी बनाने या कमाने के कार्य परिवार में ही होते थे जैसे कि गेहूँ उगाने का कार्य या आटा पीसने का कार्य। परिवार में ही जीवन जीने के सभी साधन मौजूद थे।
परंतु समय के साथ-साथ समाज में परिवर्तन आए तथा हमारे समाजों में औद्योगिकीकरण शुरू हुआ। परिवार के आर्थिक कार्य उद्योगों के पास चले गए हैं जैसे कि आटा अब चक्कियों पर पिसता है अथवा कपड़ा बड़ी-बड़ी मिलों में बनता है। इस प्रकार परिवार के आर्थिक उत्पादन के कार्य धीरे-धीरे खत्म हो गए तथा परिवार के आर्थिक कार्य और संस्थाओं के पास चले गए।
3. शैक्षिक कार्यों का परिवर्तित होना (Changes in Educational Functions)-प्राचीन समय में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य या तो गुरुकुल में होता था या फिर घर में। बच्चा अगर गुरु के पास शिक्षा लेने जाता भी था तो उसे केवल वेदों, पुराणों इत्यादि की शिक्षा ही दी जाती थी। उसे पेशे अथवा कार्य से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जा थी तथा यह कार्य परिवार द्वारा ही किया जाता था।
प्रत्येक जाति अथवा परिवार का एक परंपरागत पेशा होता था तथा उस पेशे से संबंधित गुर भी उस परिवार को पता होते थे। वह परिवार अपने बच्चों को धीरे-धीरे पेशे से संबंधित शिक्षा देता जाता था तथा बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। परंतु समय के साथ-साथ परिवार के इस कार्य में परिवर्तन आया है।
अब पेशों से संबंधित शिक्षा देने का कार्य परिवार नहीं बल्कि सरकार द्वारा खोले गए Professional Colleges, Medical Colleges, Engineering Colleges, I.I.M.’s, I.I.T.’s, I.T.I.’s Fruit करते हैं। बच्चा इनमें से पेशे से संबंधित शिक्षा ग्रहण करके अपना स्वयं का पेशा अपनाता है तथा परिवार का परंपरागत पेशा छोड़ देता है। इस प्रकार परिवार का शिक्षा देने का परंपरागत कार्य और संस्थाओं के पास चला गया है।
4. पारिवारिक एकता का कम होना (Decreasing Unity of Family)-प्राचीन समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे तथा परिवार के सभी सदस्य परिवार के हितों के लिए कार्य करते थे। वह अपने हितों को परिवार के हितों पर त्याग देते थे। परिवार के सदस्यों में पूर्ण एकता होती थी। सभी सदस्य परिवार के बुजुर्ग की बात माना करते थे तथा अपने फर्ज़ अच्छे ढंग से पूर्ण किया करते थे। परंतु समय के साथ-साथ पारिवारिक एकता में कमी आई।
संयुक्त परिवार खत्म होने शुरू हो गए तथा केंद्रीय परिवार सामने आने लग गए। परिवार के सभी सदस्यों के अपने अपने हित होते हैं तथा कोई भी परिवार के हितों पर अपने हितों का त्याग नहीं करता है। सभी के अपने-अपने आदर्श होते हैं जिस कारण कई बार तो वह घर ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार समय के साथ-साथ पारिवारिक एकता में कमी आई है।
5. सामाजिक कार्यों में परिवर्तन (Change in Social Functions)-परिवार के सामाजिक कार्य भी काफी बदल गए हैं। प्राचीन समय में परिवार सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में काफी महत्त्वपूर्ण कार्य करता था। परिवार दस्यों पर पर्ण नियंत्रण रखता था। उसकी अच्छी-बरी आदतों पर नज़र रखता था तथा उसे समय-समय पर ग़लत कार्य न करने की चेतावनी देता था। सदस्य भी परिवार के बुजुर्गों से डरते थे, जिस कारण वह नियंत्रण में रहते थे। परंतु समय के साथ-साथ व्यक्ति पर पारिवारिक नियंत्रण कम होने लग गया तथा नियंत्रण के औपचारिक साधन सामने आने लग गए जैसे कि पुलिस, सेना, न्यायालय, जेल इत्यादि।
इसके साथ प्राचीन समय में स्त्री अपने पति को परमेश्वर समझती थी तथा उसे भगवान् का दर्जा देती थी। पति की इच्छा के सामने वह अपनी इच्छा का त्याग कर देती थी। परंतु अब यह धारणा बदल गई है। अब पत्नी पति को परमेश्वर नहीं बल्कि अपना साथी अथवा दोस्त समझती है जिससे कि वह अपनी समस्याएं साझी कर सके।
पहले परिवार बच्चों का पालन-पोषण करते थे तथा बच्चों के बड़ा होने तक उनका उत्तरदायित्व निभाते थे। परंतु आजकल के समय में केंद्रीय परिवार होते हैं तथा स्त्रियां नौकरी करती हैं जिस कारण बच्चा परिवार में नहीं पलता बल्कि क्रेचों में पलता है। इस प्रकार परिवार के बहुत से सामाजिक कार्य बदल कर और संस्थाओं के पास चले गए हैं।
6. धार्मिक कार्यों में परिवर्तन (Change in Religious Functions)-प्राचीन समय में चाहे बच्चों को गुरु के आश्रम में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी तथा उसे वहीं पर वेदों, पुराणों इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी परंतु फिर भी परिवार उसे धार्मिक शिक्षा भी देता था। उसे धर्म तथा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। समय-समय पर परिवार में धार्मिक संस्कार, यज्ञ तथा अनुष्ठान होते रहते थे जिससे बच्चों को धर्म के बारे में काफी कुछ पता चलता रहता था। इस प्रकार परिवार में ही बच्चों की धार्मिक शिक्षा हो जाती थी। परंतु समय के साथ बहुत से आविष्कार हुए, की तथा विज्ञान प्रत्येक बात को तर्क पर तोलता है।
लोग विज्ञान की शिक्षा लेकर धर्म को भूलने लग गए। अब लोग प्रत्येक धार्मिक संस्कार को तर्क की कसौटी पर तोलने लग गए हैं कि यह क्यों और कैसे है। अब लोगों के पास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समय नहीं है। अब लोग धार्मिक कार्यों के लिए थोड़ा-सा ही समय निकाल पाते हैं तथा वह भी अपने समय की उपलब्धता के अनुसार। अब लोग विवाह जैसे धार्मिक संस्कार को सामाजिक उत्सव की तरह मनाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जा सके। लोग इनमें अधिक से अधिक पैसा खर्च जिस कारण धार्मिक क्रियाओं का महत्त्व कम हो गया है। इस प्रकार परिवार में धार्मिक कार्य कम हो गए हैं।
इस प्रकार इस व्याख्या को देखकर हम कह सकते हैं कि परिवार के कार्यों तथा ढांचे में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। परिवार के बहुत से कार्य और संस्थाओं के पास चले गए। चाहे यह परिवर्तन समय के साथ-साथ आए हैं परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि परिवार का व्यक्ति के जीवन में जो महत्त्व है उसका स्थान कोई और संस्था नहीं ले सकती है।
प्रश्न 15.
परिवार से सामाजिक कार्यों की व्याख्या करें।
उत्तर:
(i) बच्चों का समाजीकरण (Socialization of Children) बच्चों का समाजीकरण करने में परिवार सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। अगर बच्चा परिवार में रहकर अच्छी आदतें सीखता है तो उससे वह समाज का एक अच्छा नागरिक बनता है। बच्चे का समाज के साथ संपर्क भी परिवार के कारण ही स्थापित होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वह सबसे पहले अपने माता-पिता पर निर्भर होता है क्योंकि उसकी भूख-प्यास जैसी ज़रूरतें परिवार ही पूर्ण करता है। व्यक्ति को परिवार से ही समाज स्थिति तथा भूमिका भी प्राप्त होती है। व्यक्ति को अगर कोई पद प्रदान किया जाता है तो वह भी परिवार के कारण ही किया जाता है। इस प्रकार परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(ii) संस्कृति की सुरक्षा तथा हस्तांतरण (Protection and transmission of culture)-जो कुछ भी आज तक मनुष्य ने प्राप्त किया है वह उसकी संस्कृति है तथा यह संस्कृति परिवार के कारण ही सुरक्षित रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। यह प्रत्येक परिवार का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी-अच्छी आदतें, रीति-रिवाज, परंपराएं, मूल्य, आदर्श इत्यादि सिखाए। बच्चे चेतन या अचेतन मन से यह सब धीरे-धीरे ग्रहण करते हैं।
वह वही सब कुछ सीखते तथा ग्रहण करते हैं जो वह अपने माता-पिता को करते हुए देखते हैं। प्रत्येक परिवार के कुछ आदर्श, परंपराएं तथा रीति-रिवाज होते हैं तथा परिवार इन सभी चीज़ों को धीरे-धीरे बच्चों को प्रदान करता जाता है। इस प्रकार बच्चा इन सभी को ग्रहण करता है तथा परिवार के आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार परिवार समाज की संस्कति को सरक्षित रखता है तथा उसे एक पीढी से दसरी पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित करती है।।
(iii) व्यक्तित्व का विकास (Development of personality) परिवार में रहकर बच्चा बहुत सी नई आदतें सीखता है, बहुत-से नए आदर्श, मूल्य इत्यादि ग्रहण करता है जिससे उसका समाजीकरण होता रहता है। परिवार व्यक्ति की ग़लत प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, उसे कई प्रकार के उत्तरदायित्व सौंपता है, उसमें अच्छी आदतें डालता है तथा उसमें स्वः का विकास करने में सहायता करता है।
परिवार में रहकर ही बच्चे में बहुत-से गुणों का विकास होता है जैसे कि प्यार, सहयोग, अनुशासन, हमदर्दी इत्यादि तथा यह सब कुछ उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे को परिवार में रहकर कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है जिससे उसका व्यक्तित्व और विकसित हो जाता है तथा वह समाज में रहने के तौर-तरीके सीखता जाता है।
(iv) व्यक्ति को स्थिति प्रदान करना (To provide status to individual)-परिवार में बच्चे को यह पता चल जाता है कि परिवार में और समाज में उसकी स्थिति क्या है तथा उसे कौन-सी भूमिका निभानी है। प्राचीन समाजों में तो बच्चे को प्रदत्त स्थिति प्राप्त हो जाती थी अर्थात् जिस प्रकार के परिवार में वह जन्म लेता था उसे उसकी ही स्थिति प्राप्त हो जाती थी।
उदाहरण के तौर पर राजा के परिवार में पैदा हुए बच्चे को राजा जैसा सम्मान प्राप्त हो जाता था तथा निर्धन के घर पैदा हुए बच्चे को न के बराबर सम्मान प्राप्त होता था। निर्धन व्यक्ति के बच्चों की स्थिति हमेशा निम्न होती थी। इस प्रकार परिवार के कारण ही व्यक्ति को समाज में स्थिति प्राप्त होती थी। चाहे आधुनिक समय में व्यक्ति स्थिति को अर्जित करने में लग गए हैं परंतु फिर भी परंपरागत समाजों में आज भी व्यक्ति को प्रदत्त स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार परिवार व्यक्ति को स्थिति प्रदान करता है।
(v) व्यक्ति पर नियंत्रण रखना (To keep control on individual)-अगर हम सामाजिक नियंत्रण के साधनों की तरफ देखें तो परिवार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि परिवार ही व्यक्ति को नियंत्रण में रहना सिखाता है। परिवार बच्चे में अच्छी-अच्छी आदतें डालता है ताकि उसमें ग़लत आदतों का विकास न हो सके। बच्चे पर माता पिता नियंत्रण रखते हैं, उस के झूठ बोलने पर उसे डाँटते हैं, उसे बड़ों के साथ सही प्रकार से बोलने के लिए कहते हैं, उसे समाज द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में बताते हैं ताकि वह समाज का ज़िम्मेदार नागरिक बन सके तथा समाज में उनके परिवार का सम्मान और बढ़ जाए। परिवार में रहकर बच्चा अनुशासन में रहना सीखता है तथा अपने व्यवहार और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है।
अगर बच्चा परिवार के सदस्यों के साथ ही ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करेगा तो वह समाज के और सदस्यों के साथ ठीक ढंग से कैसे व्यवहार करेगा। बच्चा परिवार के दूसरे सदस्यों को कार्य करता देखकर बहुत-सी बातें सीखता है। अगर परिवार के सदस्य ग़लत कार्य करेंगे तो बच्चा भी वह सब कुछ ग्रहण करेगा परंतु अगर परिवार के सदस्य ग़लत कार्य न करके अच्छी बातें करेंगे तो बच्चे भी अच्छी बातें करेंगे तथा वे नियंत्रण में रहेंगे। इस प्रकार परिवार सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।
(vi) विवाह करने में सहायता प्रदान करना (To give help in settling marriage) अगर कोई व्यक्ति विवाह करना चाहे तो सबसे पहले उससे परिवार, खानदान या वंश के बारे में पूछा जाता है ताकि उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके। अगर वह अच्छे परिवार से संबंध रखता है तो विवाह करने में कोई परेशानी नहीं होती परंतु अगर वह किसी निम्न श्रेणी के परिवार से संबंध रखता है तो विवाह करने में काफ़ी समस्या आती है। परिवार अपने बच्चों का विवाह करवाना अपना कर्तव्य समझता है ताकि वंश आगे बढ़ सके। अगर परिवार यह कर्तव्य पूर्ण नहीं करता तो उसे समाज में अच्छी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसलिए परिवार व्यक्ति का विवाह करने में सहायता प्रदान करता है।
(vii) पेशा प्रदान करना (To provide occupation)-चाहे आजकल के समय में तो परिवार का यह कार्य काफ़ी कम हो गया है परंतु प्राचीन समाजों में तथा परंपरागत समाजों में भी यह कार्य काफ़ी महत्त्वपूर्ण होता है। भारतीय समाज में प्राचीन समय में जाति प्रथा प्रचलित थी जिसमें चार महत्त्वपूर्ण वर्ण हुआ करते थे-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।
प्रत्येक वर्ग में पैदा हुआ बच्चा केवल अपने ही वर्ण का पेशा अपना सकता था अर्थात् ब्रा परिवार में पैदा हुआ बच्चा केवल ब्राह्मण का ही कार्य कर सकता था तथा शूद्र परिवार में घर पैदा हुआ बच्चा केवल उस परिवार का ही कार्य अपना सकता था। चाहे आधुनिक समय में यह कार्य कम हो गया है तथा लोक परिश्रम करके अपनी मर्जी का पेशा अपना रहे हैं परंतु फिर भी व्यापारियों, दुकानदारों के बच्चे अपने परिवार का पेशा ही अपनाते बाह्मण हैं।
(viii) शिक्षा देना (To give education)-जब बच्चा पैदा होता है तो उसे समाज में रहने के नियम पता नहीं होते हैं। उसमें पशु प्रवृत्ति होती है तथा वह प्रत्येक चीज़ को अपना समझता है। परिवार ही उस की पशु प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखता है तथा उसे समाज में रहने के नियम सिखाता है। इस प्रकार बच्चे को सबसे पहली शिक्षा परिवार में ही प्राप्त होती है। धर्म की शिक्षा, पेशे की शिक्षा, नियम सीखने की शिक्षा इत्यादि जैसी शिक्षा बच्चे को परिवार में ही मिलती है। चाहे आजकल के समय में औपचारिक शिक्षा देने का कार्य और संस्थाओं के पास चला गया है, परंतु फिर भी बच्चे को शिक्षा देने का कार्य परिवार ही करता है।
प्रश्न 16.
नातेदारी क्या होती है? इसके प्रकार बताओ।
उत्तर:
मानव इतिहास के आरंभिक चरणों से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मनुष्यों ने समूहों एवं झुंडों में रहना आरंभ किया। उसके द्वारा निर्मित समूह ही नातेदारी व्यवस्था के उद्विकास का प्रथम चरण था। उद्विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही यह वर्तमान स्वरूप में विकसित हुई।
समाजों की पृष्ठभूमि, सामाजिक संस्कृति, आर्थिक दशाओं द्वारा नातेदारी का स्वरूप एवं आकार निर्धारित किया जाता है। नातेदारी सर्वव्यापी संस्था है। लेकिन सभी समाजों में इसका स्वरूप, रीतियां, संबंधों की घनिष्ठता तथा घनिष्ठ संबंधियों की संख्या में अंतर पाया जाता है। नातेदारी के लिये बंधुत्व, संगोत्रता एवं स्वजनता आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है।
नातेदारी व्यवस्था का अर्थ (Meaning of Kinship System) रैडक्लिफ ब्राऊन के शब्दों में, “नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिये स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है।”
लैवी स्ट्रास के अनुसार, “नातेदारी व्यवस्था विचारों की एक निरंकुश व्यवस्था है। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक संबंधों पर आधारित हों। नातेदारी की यह परिभाषा ‘तिनिक’ ने मानव शास्त्र के शब्द कोष में दी है।” ‘फ़ॉक्स’ ने अपनी कृति ‘नातेदारी एवं विवाह’ में लिखा है “नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात् वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है।”
डॉ० रिवर्स ने अपनी पुस्तक ‘सामाजिक संगठन’ में लिखा है संगोत्रता (बंधुत्व) की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित एवं वर्णित की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी ऐसे संबंधियों के बीच संबंधों की व्यवस्था होती है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। वंशावली संबंध परिवार के द्वारा विकसित होते हैं।
नातेदारी व्यवस्था के प्रकार/आधार
(Types/Bases of Kinship)
नातेदारी व्यवस्था समाज में दो आधारों पर विकसित होती है-
- रक्तमूलक नातेदारी (Consenguineous Kinship)
- विवाहमूलक नातेदारी (Affinal Kinship)
1. रक्तमूलक नातेदारी (Consenguineous Kinship)-रक्तमूलक नातेदारी वह होती है, जिसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, जो आपस में रक्त द्वारा संबंधित होते हैं। जैसे माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-ताया-दादा-पिता, पुत्र-पौत्र इत्यादि सब एक-दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। रक्त संबंध के भी दो मूलाधार होते हैं-
माता के वंश के सभी सदस्य व्यक्ति के रक्त संबंधी होते हैं। इसी प्रकार पिता के रिश्तेदार भी आपस में रक्त संबंधी होते हैं। चाचा, ताया, दादा आदि पिता के वंश तथा मामा, नाना, नानी आदि माता के वंश के रक्त संबंधी हैं।
रक्त संबंधी दो प्रकार के होते हैं-
- रेखीय नातेदारी (Lineal Kinship)
- क्षैतिज नातेदारी (Collateral Kinship)।
1. रेखीय नातेदारी में संबंधियों के बीच रक्त संबंध एक रेखा के रूप में होता है, जैसे-परदादा, दादी, पिता, पुत्र, पौत्र इत्यादि। क्षैतिज संबंधी वे होते हैं, जिनका सीधा रक्त संबंध नहीं होता। फिर भी एक ही पूर्वज के साथ संबंधित होने के कारण आपस में रक्त संबंधी होते हैं; जैसे चाचा, ताया, भतीजी इत्यादि। रक्त संबंध वास्तविक के अतिरिक्त काल्पनिक भी होता है। जैसे कई जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है।
वहां जो भाई पत्नी के गर्भवती होने पर तीर-कमान का संस्कार पूरा करता है, वही होने वाली संतान का पिता माना जाता है। इसी तरह किसी व्यक्ति के द्वारा गोद ली गई संतान भी उसकी अपनी संतान मानी जाती है। अतः यह आवश्यक नहीं कि पिता व संतान का आपस में जैवकीय संबंध (Biological relationship) हो। फिर भी वह रक्त संबंधी माने जाते हैं।
2. विवाहमूलक नातेदारी (Affinal Kinship)-विवाहमूलक नातेदारी ऐसी नातेदारी है जो दो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति द्वारा स्थापित की जाती है। विवाह के द्वारा पति-पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं बनते बल्कि पत्नी के सब रिश्तेदार पति के लिये और पति के सब नातेदार पत्नी के लिये विवाह संबंधी होते हैं। अतः विवाह द्वारा नातेदारी में लगभग दुगुणी वृद्धि हो जाती है। विवाहमूलक नातेदारी में सास, ससुर, जीजा, ननद, साला, साली, बहनोई, ज्येष्ठ, बहु, देवर आदि रिश्तेदार सम्मिलित होते हैं।
प्रश्न 17.
आज के समय में नातेदारी का क्या महत्त्व है?
उत्तर:
नातेदारी की भूमिका एवं महत्त्व (Role and Importance of Kinship)-नेलसन ग्रेबन ने अपनी कृति “Reading in Kinship’ में लिखा है, “नातेदारी व्यवस्था सर्वव्यापी है। सामाजिक संगठन को समझने के लिये नातेदारी संस्थाओं का ज्ञान महत्त्वपूर्ण है।” डॉ० रिवर्स कहते हैं, “अनेक भारतीय मानव शास्त्रियों (Anthropologists) ने नातेदारी के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर मानव शास्त्रीय ज्ञान को समृद्ध बनाया है।” उन्होंने नातेदारी के मानवशास्त्र के अंतर्गत विकसित किये माडलों (Models) को नातेदारी के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिये प्रयोग किया। नातेदारी को भूमिका एवं महत्त्व का संक्षिप्त वर्णन विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अधोलिखित है
1. परिस्थति निर्धारण (Determination of Status)-नातेदारी व्यक्ति की जन्म से सामाजिक प्रस्थिति को निर्धारित करती है। उच्च परिवार एवं नातेदारी से संबंधित व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति उच्च होती है। उदाहरणार्थ राजनीति में मंत्री, एम० एल० ए०, एम० पी० नौकरी में उच्च पद पर कार्यरत तथा उच्च स्तर के वाणिज्य व्यापार करने वालों के परिवार जनों एवं रिश्तेदारों को उच्च प्रस्थिति प्राप्त होती है। चाहे व्यक्ति की निजी उपलब्धियां भी कम हों।
2. वंश एवं उत्तराधिकार का निर्धारण (Determination of Descent and Inheritance)-वंश व्यक्ति का मूल (Root) होता है। परिवार, वंश, गोत्र, मातदल नातेदारी के ही अंग हैं। किस व्यक्ति को अपने पूर्वजों की संपत्ति, चल-अचल, भौतिक-अभौतिक का हस्तांतरण होगा। कौन व्यक्ति उत्तराधिकारी होगा तथा उत्तराधिकार के कितने भाग का उसे अधिकार होगा, ये सब बातें नातेदारी के सदस्यों में विभिन्न नियमों द्वारा तय की जाती हैं।
लूसी मेयर ने अपनी कृति ‘सामाजिक विज्ञान की भूमिका’ में इस संबंध में लिखा है, “किसी व्यक्ति का समाज में स्थान, उसके अधिकार और कर्तव्य, संपत्ति पर उसका दावा अधिकतर दूसरे सदस्यों के साथ, उसके जन्मजात संबंधों पर निर्भर करते हैं। ऐसे समाज में संगठन के चाहे जो भी सिद्धांत हों प्राथमिक समूह व तथा उत्तराधिकार निर्धारित किया जाता है।”
3. समाजीकरण (Socialization)-परिवार एवं परिवारों की समूह नातेदारी व्यक्ति के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां (Agencies) हैं। नवजात शिशु सर्वप्रथम अपनी नातेदारी माता-पिता इत्यादि के संपर्क में आता है। वहीं से वह जैविकीय प्राणी (Biological Being) से सामाजिक प्राणी बनना प्रारंभ करता है। संबंधी उसे चलना, बोलना, भाषा, सामाजिक मूल्य तथा व्यवहार के तरीके सिखाते हैं।
4. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)-अपने सदस्यों को नातेदारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाता है। व्यक्ति को जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार वह समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा लेता है। लेकिन कई बार असफलता ही उसके हाथ लगती है। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य संबंधी ही उसे ढांढस बंधवाते हैं। आकस्मिक मृत्यु, आपदा, विपत्ति दुःख, असफलता आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में नातेदारी व्यक्ति को उभारने में सहायता करता है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको सहयोग भी देती है।
5. आर्थिक हितों की सुरक्षा (Safeguard of Economic Interests)-नातेदार व्यक्ति के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। भारतीय समाज में तो इस क्षेत्र में नातेदारी का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि नातेदारी व्यक्ति को जातिगत व्यवसाय सीखने तथा अपनाने में सहायता करती है। लूसी मेयर द्वारा नातेदारी व्यक्ति के आर्थिक हितों की सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में लिखती है, “विभिन्न समाजों में स्वीकृत बंधुत्व के बंधन लोगों को खेती तथा जायदाद पर अधिकार, समान हितों की पूर्ति में परस्पर सहायता तथा दूसरों पर आधिपत्य प्रदान करते हैं। प्रभुता प्राप्त लोगों पर यह दायित्व रहता है कि वे आश्रितों का कल्याण करें। आश्रितों का धर्म आज्ञा पालन है। सभी लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे अवसरों पर जहां बंधुत्व (नातेदारी) की मान्यता का प्रश्न है परस्पर सहयोग करें।”
6. मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार (Basis of Anthropological Knowledge)-विश्वभर के प्रमुख मानव शास्त्रियों के प्रारंभिक अध्ययन नातेदारी से ही संबंधित थे। उन्होंने सामाजिक संरचना की इस आधारभूत इकाई का पर्याप्त ज्ञान एकत्रित किया। मैलीनोवस्की, ब्राऊन, मार्गन, लौवी तथा हैनरीमैन आदि मानव शास्त्री उनमें से प्रमुख हैं। इन समाज शास्त्रियों के अध्ययनों से विवाह, परिवार एवं नातेदारी के उदविकास के विभिन्न चरणों का ज्ञान होना प्राप्त होता है।
7. सामाजिक संरचना को समझने में सहायक (Helpful in Understanding Social Structure) सामाजिक संरचना विशेषतः भारतीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए नातेदारी के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान आवश्यक है। विभिन्न रिश्तेदार आपस में विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं। इसके लिए नातेदारी की रीतियों को समझने की आवश्यकता है। ससुर के समक्ष आने पर बहू द्वारा एकदम चूंघट डाल लेना, पत्नी द्वारा पति के निकटतम संबंधी का नाम न लेना इत्यादि सामाजिक वास्तविकताओं को तभी समझा जा सकता है, यदि नातेदारी व्यवस्था का ज्ञान हो।
8. सामाजिक नियंत्रण (Social Control) नातेदारी सामाजिक नियंत्रण में महत्त्वपर्ण भमिका अभिनीत करती है। विभिन्न रिश्तेदारों को कैसे संबोधित किया जाए, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, आदि मूल्यों को नातेदारी अनुपालना सुनिश्चित करवाती है। नातेदारी होने के अहसास मात्र से व्यक्ति कई अवांछनीय कार्य नहीं करते हैं।
प्रत्येक समाज में नातेदारी व्यवस्था पायी जाती है। लेकिन किन तथा कितने व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, ये प्रत्येक समाज में प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करता है। भारतीय समाज में साधारणतया नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत पश्चिमी समाज की अपेक्षा कहीं अधिक संबंधी आते हैं। संबंधी का स्वरूप एवं क्षेत्र सामाजिक मूल्य तय करते हैं। नातेदारी व्यवस्था निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती है तथा समाज में संगठन, संतुलन, भाईचारे आदि को बढ़ावा देती है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()