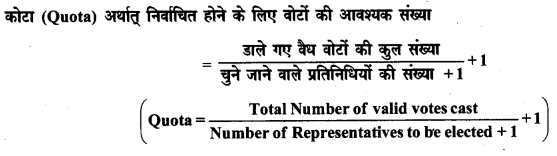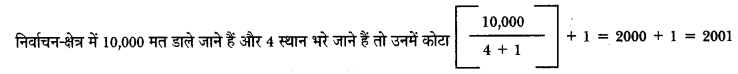Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 2 भारतीय संविधान में अधिकार Important Questions and Answers.
Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 2 भारतीय संविधान में अधिकार
अति लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
सर्वप्रथम मानवाधिकारों की घोषणा कब और कहाँ हुई थी?
उत्तर:
सर्वप्रथम मानवाधिकारों की घोषणा 1789 ई० में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में हुई थी।
प्रश्न 2.
भारत में सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा मौलिक अधिकारों की माँग की गई?
उत्तर:
भारत में सर्वप्रथम 1895 ई० में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मौलिक अधिकारों की माँग की गई।
प्रश्न 3.
भारतीय संविधान द्वारा दिए अधिकारों को मौलिक कहने के कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर:
(1) अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात् संविधान में स्थान दिया गया है और इनमें विशेष संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता,
(2) ये अधिकार – व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं, जिनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा।
प्रश्न 4.
दक्षिण अफ्रीका के संविधान में वर्णित किन्हीं दो मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- गरिमा का अधिकार,
- स्वास्थ्य की रक्षा, रोटी, पानी तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।
प्रश्न 5.
मूल अधिकारों को संविधान में रखने के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- सत्तारूढ़ दल के अत्याचार से सुरक्षा करने हेतु तथा,
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए।
प्रश्न 6.
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
- मौलिक अधिकार पूर्ण तथा निरंकुश नहीं हैं,
- संसद मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकती है।
प्रश्न 7.
‘कानून के समक्ष समानता’ से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता और समस्त व्यक्ति कानून के सामने बराबर होते हैं।

प्रश्न 8.
‘कानून के समक्ष संरक्षण’ से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
कानून के समक्ष संरक्षण से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का एक-समान व्यवहार होना।
प्रश्न 9.
भारतीय संविधान में वर्णित ‘समानता के अधिकार’ के कोई दो अपवाद लिखिए।
उत्तर:
- विदेशी राज्यों के मुखियाओं और राजनायिकों के विरुद्ध भारतीय कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती,
- राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान कोई फौजदारी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।
प्रश्न 10.
भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार के किन्हीं दो अपवादों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- ये अधिकार शत्रु-देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे,
- निवारक नजरबन्दी के अधीन की गई गिरफ्तारी के सन्दर्भ में भी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार की व्यवस्थाएँ लागू नहीं होंगी।
प्रश्न 11.
‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) का क्या अर्थ है?
उत्तर:
हैबियस कॉरपस’ लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ‘शरीर हमारे सामने पेश करो।’ इस लेख द्वारा न्यायालय बन्दी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बन्दी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, जिससे न्यायालय यह निर्णय कर सके कि किसी व्यक्ति को बन्दी बनाए जाने के कारण वैध हैं या अवैध । यदि बन्दी बनाने के कारण अवैध हैं तो उसे मुक्त करने संबंधी लेख जारी किया जाता है।
प्रश्न 12.
‘परमादेश लेख (Writ of Mandamus) से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
‘मेण्डेमस’ शब्द लेटिन भाषा का है जिसका अर्थ है ‘हम आज्ञा देते हैं। यह लेख न्यायालय उस समय जारी करता है, जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने सार्वजनिक दायित्व का निर्वाह न कर रही हो और जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो।
प्रश्न 13.
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की आलोचना के कोई दो आधार लिखिए।
उत्तर:
- संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों पर बहुत अधिक प्रतिबंध हैं, जिसके फलस्वरूप साधारण व्यक्ति इन्हें समझने में प्रायः असमर्थ-सा रहता है,
- मौलिक अधिकारों की भाषा कठिन एवं अस्पष्ट है जिसे साधारण एवं अशिक्षित व्यक्ति समझ नहीं पाता।
प्रश्न 14.
मौलिक अधिकारों की कोई दो उपयोगिताएँ लिखिए।
उत्तर:
- मौलिक अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं,
- मौलिक अधिकारों द्वारा समाज में सामाजिक समानता की स्थापना होती है।
प्रश्न 15.
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब और कौन-से भाग में जोड़ा गया?
उत्तर:
भारतीय संविधान में सन् 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 51-A में जोड़ा गया।
प्रश्न 16.
भारतीय संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय झण्डे तथा गान का सम्मान करना,
- भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखण्डता को बनाए रखना और सुरक्षित रखना।।
प्रश्न 17.
भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक कर्तव्यों के कोई दो महत्त्व लिखिए।
उत्तर:
- मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के आदर्श एवं पथ-प्रदर्शक हैं,
- मौलिक कर्त्तव्य मूल अधिकारों की प्राप्ति में सहायक हैं।
प्रश्न 18.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोई दो कार्य लिखिए।
उत्तर:
- यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करता है,
- यह मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करता है।
प्रश्न 19.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का तात्पर्य यह है कि ये सिद्धान्त संविधान के द्वारा आगामी सरकारों के लिए कुछ नैतिक निर्देश हैं। ये सिद्धान्त इस प्रकार के आदेश हैं जिन पर आगामी सरकारों को जनता के हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा दी गई है।
प्रश्न 20.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों के कोई दो लक्षण लिखिए।
उत्तर:
- ये राज्य की शासन-व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त हैं,
- ये सिद्धान्त न्याय योग्य नहीं हैं।
प्रश्न 21.
राज्य-नीति के कोई दो समाजवादी निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- राज्य ऐसा प्रयास करें कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीयकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुँचे,
- स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।
प्रश्न 22.
राज्य-नीति के कोई दो गाँधीवादी निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
(1) अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जिनसे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें,
(2) अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य समाज के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा कबीलों की शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाएगा।
प्रश्न 23.
राज्य-नीति के कोई दो उदारवादी निदेशक सिद्धान्त लिखिए।
उत्तर:
- राज्य समस्त भारत में समान आचार-संहिता लागू करने का प्रयत्न करेगा,
- राज्य ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्त्व रखने वाले स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की रक्षा करेगा और उनको नष्ट होने से बचाएगा।
प्रश्न 24.
राज्य-नीति के किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना,
- राष्ट्रों के मध्य उचित व सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रयास करना।
प्रश्न 25.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की आलोचना के कोई दो आधार बताइए।
उत्तर:
- निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कानूनी शक्ति का अभाव है,
- 20वीं शताब्दी में लागू होने वाले निदेशक सिद्धान्त 21वीं शताब्दी में भी उपयोगी होंगे, यह आवश्यक नहीं है।
प्रश्न 26.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों के कोई दो महत्त्व लिखिए।
उत्तर:
- ये सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे,
- इन सिद्धान्तों से सरकार की नीतियों में निरन्तरता तथा स्थिरता सम्भव होगी।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन-से मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
उत्तर:
मौलिक अधिकार उन सुविधाओं, स्वतन्त्रताओं तथा अधिकारों को कहते हैं जो एक व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। ये वे मूल अधिकार हैं जिनका प्रयोग किए बिना व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक लोकतन्त्रीय राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेद-भाव के कुछ मौलिक अधिकार देता है। भारतीय संबिधान द्वारा भी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं-
- समानता का अधिकार,
- स्वतन्त्रता का अधिकार,
- शोषण के विरुद्ध अधिकार,
- धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार,
- सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार,
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
प्रश्न 2.
भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का महत्त्व बताइए।
उत्तर:
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का बहुत महत्त्व है। ये देश के सभी नागरिकों को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानून के सामने समानता पर बल देते हैं। ये नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान करते हैं जिनके प्रयोग से वे अपने जीवन की उन्नति तथा विकास कर सकते हैं।
इन अधिकारों से भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का भी संकेत मिलता है। मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं और उसे मनमानी करने से रोकते हैं। ये अधिकार सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए भारत में सामाजिक-आर्थिक लोकतन्त्र के विकास में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करते हैं।

प्रश्न 3.
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कोई पाँच विशेषताएँ बताएँ।।
उत्तर:
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की पाँच विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार बहुत ही व्यापक तथा विस्तृत हैं,
- मौलिक अधिकार न्याय-संगत हैं। इसका अर्थ यह है कि इनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्यायालय में जाकर न्याय माँगने का अधिकार है,
- मौलिक अधिकार सीमित हैं। इनके प्रयोग पर कुछ सीमाएँ लगी हुई हैं,
- मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं,
- संकटकाल में मौलिक अधिकारों को निलम्बित (Suspend) किया जा सकता है।
प्रश्न 4.
भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार की व्याख्या करो।
अथवा
भारतीय संविधान के अनच्छेद 14-18 में दिए गए समानता के अधिकार का वर्णन करो।
उत्तर:
‘समानता का अधिकार’ का वर्णन संविधान की धारा 14-18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 15 के अनुसार नागरिकों में जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा जन्म-स्थान आदि के आधार पर सभी प्रकार के भेद-भावों को समाप्त कर दिया गया है।
अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के क्षेत्र में समानता प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 17 के अनुसार देश में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इसके प्रयोग को कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है।
अनुच्छेद 18 द्वारा सैनिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है।
प्रश्न 5.
संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत नागरिकों को कौन-कौन-सी स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं? अथवा भारतीय संविधान में दी गई विभिन्न मूल स्वतन्त्रताओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत नागरिकों को दी गई स्वतन्त्रताएँ इस प्रकार हैं-
- भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता,
- शान्तिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सभा करने की स्वतन्त्रता,
- समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतन्त्रता,
- देश के किसी भी भाग में घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता,
- देश में किसी भी स्थान पर बसने की स्वतन्त्रता,
- कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतन्त्रता।
प्रश्न 6.
मौलिक स्वतन्त्रताओं पर किन आधारों पर तार्किक प्रतिबन्ध (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं?
उत्तर:
अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत दी गई स्वतन्त्रताओं पर निम्नलिखित तार्किक प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं-
(1) संसद भारत की प्रभुसत्ता, अखण्डता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इन स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबन्ध लगा सकती है,
(2) संसद विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए इन स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबन्ध लगा सकती है,
(3) संसद सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता, न्यायालय का अपमान, मान-हानि व हिंसा के लिए उत्तेजित करना आदि के आधारों पर इन स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबन्ध लगा सकती है,
(4) राज्य जनता के हितों और अनुसूचित कबीलों के हितों की सुरक्षा के लिए इन स्वतन्त्रताओं पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।
प्रश्न 7.
शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार व्यक्तियों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं ली जा सकती। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक दशा से अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता और उसे कोई भी काम उसकी इच्छा के विरुद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी ऐसे कारखाने या खान में नौकर नहीं रखा जा सकता, जहाँ उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।
प्रश्न 8.
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में की गई व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
(1) संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा समाप्त करता हो।
(2) मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं और हम उनकी रक्षा के लिए न्यायालयों में जा सकते हैं। न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकते हैं।
(3) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के पास पुनर्निरीक्षण की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय संसद तथा राज्य विधानमण्डल के कानूनों को और राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के आदेश को रद्द कर सकते हैं, यदि वे कानून या आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों।
प्रश्न 9.
संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
सवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति की रक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है।
यदि सरकार हमारे किसी मौलिक अधिकार को लागू न करे या उसके विरुद्ध कोई काम करे तो उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है और न्यायालय द्वारा उस अधिकार को लागू करवाया जा सकता है या उस कानन को रद्द कराया जा सकता है। उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस सम्बन्ध में कई प्रकार के लेख (Writs) जारी करने का अधिकार है।
प्रश्न 10.
सवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत न्यायपालिका किस प्रकार के आदेशों को जारी कर सकती है?
उत्तर:
मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका निम्नलिखित आदेश जारी कर सकती है-
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख,
- परमादेश का आज्ञा-पत्र,
- मनाही आज्ञा-पत्र,
- उत्प्रेषण लेख तथा
- अधिकार-पृच्छा लेख।
प्रश्न 11.
‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख’ (Writ of Habeas Corpus) तथा ‘परमादेश लेख’ (Writ of Mandamus) पर नोट लिखिए।
उत्तर:
1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख-‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ शब्द लेटिन भाषा के शब्द ‘हेबियस कॉर्पस’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है-‘हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो’ (Let us have the body.) इस आदेश के अनुसार न्यायालय किसी अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी ढंग से बन्दी बना रखा हो, आज्ञा दे सकता है कि कैदी को समीप के न्यायालय में उपस्थित किया जाए, ताकि उसकी गिरफ्तारी के कानून के औचित्य या अनौचित्य का निर्णय किया जा सके। अनियमित गिरफ्तारी की दशा में न्यायालय उसको स्वतन्त्र करने का आदेश दे सकता है।
2. ‘परमादेश’ लेख-‘परमादेश लेख’ लेटिन भाषा के शब्द ‘मैण्डमस’ से लिया गया है। जिसका अर्थ है-‘हम आदेश देते हैं। (We Command.) इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी, संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाधित कर सकता है। इस आदेश द्वारा न्यायालय राज्य के कर्मचारियों से ऐसे कार्य करवा सकता है जिनको वे किसी कारण से न कर रहे हों तथा जिनके न किए जाने से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो।
प्रश्न 12.
अधिकार-पृच्छा लेख (Writ of Quo-Warranto) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
अधिकार-पृच्छा लेख का अर्थ है ‘किसके आदेश से’ अथवा ‘किस अधिकार से’। यह आदेश उस समय जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने का दावा करता हो, जिसको करने का उसको अधिकार न हो। इस आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई पद ग्रहण करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है और उक्त पद के रिक्त होने की तब तक के लिए घोषणा कर सकता है, जब तक कि न्यायालय द्वारा कोई निर्णय न दिया जाए।
प्रश्न 13.
संकटकाल में मौलिक अधिकारों के स्थगन पर एक नोट लिखें।
उत्तर:
संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि जब अनुच्छेद 352 तथा 356 के अन्तर्गत संकटकालीन व्यवस्था की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार तभी स्थगित किए जा सकते हैं, जब संकटकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण हो, न कि शस्त्र-विद्रोह के आधार पर।
राष्ट्रपति संकटकाल में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा लेने के अधिकार को समस्त भारत या उसके किसी भाग में स्थगित कर सकता है, परन्तु अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार को लागू करवा अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 14.
‘निवारक नजरबन्दी’ (Preventive Detention) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
किसी भी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा को भंग किए जाने के सन्देह पर बन्दी बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की ‘निजी स्वतन्त्रता’ प्राप्त नहीं होती, परन्तु यदि उसे दो महीने से अधिक नजरबन्द रखना हो, तो ऐसा सलाहकार बोर्ड के परामर्श पर ही किया जा सकता है। निवारक नजरबन्दी में बन्दी बनाए गए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाना आवश्यक है।

प्रश्न 15.
सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में किया गया है। इसके अन्तर्गत-
(1) सभी नागरिकों को अपनी भाषा, धर्म व संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का पूरा अधिकार है,
(2) भाषा अथवा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार है। इस प्रकार की संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करेगा,
(3) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा स्थापित अथवा सहायता से चलाए जाने वाले शिक्षा-संस्थान में प्रवेश देने में जाति, धर्म, वंश, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर मनाही नहीं की जा सकती।
प्रश्न 16.
भारतीय संविधान में दिए गए पाँच मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर भारतीय संविधान में दिए गए पाँच मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं
- प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रीय झण्डे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे।
- नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन के उद्देश्यों को स्मरण तथा प्रफुल्लित करें।
- प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह भारत की प्रभुसत्ता, एकता व अखण्डता का समर्थन और रक्षा करे।
- नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करें तथा राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के समय भाग लें।
- लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना।
प्रश्न 17.
मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्त्व है?
उत्तर:
मौलिक कर्तव्यों का विशेष महत्त्व है। मौलिक कर्त्तव्य नागरिक को आदर्श बनाते हैं तथा उनमें जागरूकता उत्पन्न करते हैं। मौलिक कर्त्तव्य नागरिकों का दृष्टिकोण व्यापक बनाते हैं और नागरिकों में संविधान का पालन, देश की रक्षा, एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने की भावना पैदा करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का पालन करके लोकतन्त्र को सफल बनाया जा सकता है।
इसके फलस्वरूप व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा विकास के साथ-साथ समाज और देश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि यदि लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख लेंगे तो हम शीघ्र ही एक शान्तिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण क्रान्ति देख सकेंगे। अतः मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अंकित किए जाने से नागरिकों को यह ध्यान में रहेगा कि अधिकारों के साथ-साथ उनके कुछ कर्त्तव्य भी हैं।
प्रश्न 18.
संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की आलोचना कीजिए।
उत्तर:
संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की आलोचना निम्नलिखित तथ्यों के अन्तर्गत की जा सकती है
1. कुछ मौलिक कर्त्तव्य अस्पष्ट हैं-मौलिक कर्तव्यों का विवरण देते हुए संविधान में कुछ अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनकी मनमाने ढंग से व्याख्या की जा सकती है; जैसे मिली-जुली संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अन्वेषण व सुधार की भावना।
2. दण्ड की भावना का अभाव मौलिक कर्त्तव्यों के पीछे दण्ड की भावना का अभाव है। इसी संदर्भ में स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिए और इसके लिए संसद द्वारा उचित कानून का निर्माण करना चाहिए।
3. केवल उच्च आदर्श मौलिक कर्तव्यों की आलोचना तीसरे स्थान पर की जा सकती है कि ये मात्र उच्च आदर्श प्रस्तुत करते. हैं। भारत की अंधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जो इन उच्च आदर्शों को समझने में असमर्थ है।
4. संविधान के तीसरे अध्याय में सम्मिलित होने चाहिएँ मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अध्याय चार में शामिल किया गया है, जबकि इन्हें मौलिक अधिकारों वाले अध्याय तीन में ही रखा जाना चाहिए, व कर्तव्य अच्छे लगते हैं।
प्रश्न 19.
भारतीय संविधान में दिए गए राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का स्वरूप (प्रकृति) क्या है?
रतीय संविधान के निर्माता भारत को एक आदर्श कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने सरकार की नीति तथा शासन को सही दिशा देने के लिए संविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों को शामिल किया। ये सिद्धान्त सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए हैं और ये न्यायसंगत नहीं हैं।
यदि सरकार इनमें से किसी भी सिद्धान्त को लागू नहीं करती, तो भी नागरिकों को न्यायालय में जाकर सरकार के विरुद्ध न्याय माँगने का अधिकार नहीं है। ये सरकार को सकारात्मक निर्देश हैं और यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो जनमत उस सरकार के विरुद्ध हो जाएगा। ऐसी सरकार के अगले चुनावों में जीतने की सम्भावना नहीं होगी।
प्रश्न 20.
हमारे संविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित अध्याय का क्या महत्त्व है? अथवा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का महत्त्व बताएँ।
उत्तर:
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का महत्त्व इस प्रकार है-
(1) संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इन सिद्धान्तों के लागू करने से भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है,
(2) संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने की जो घोषणा की गई है, ये सिद्धान्त उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं,
(3) ये सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की स्थापना में सहायता करते हैं,
(4) सरकारें जब इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर अपनी नीति का निर्माण करेंगी, तो समान कानूनों का निर्माण होगा, जिससे राष्ट्रीय एकता की स्थापना होगी,
(5) ये सिद्धान्त जनता के पास सरकार की सफलताओं को जाँचने की कसौटी है।
प्रश्न 21.
42वें संशोधन द्वारा निदेशक सिद्धान्तों में कौन-से नए सिद्धान्त जोड़े गए हैं ?
उत्तर:
- राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि बच्चों को स्वतंत्र और प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण में अपने विकास के लिए अवसर और सुविधाएँ प्राप्त हों,
- राज्य ऐसी कानून प्रणाली के प्रचलन की व्यवस्था करेगा जो समान अवसर के आधार पर न्याय का विकास करे,
- राज्य कानून या अन्य ढंग से श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदारी बनाने के लिए पग उठाएगा,
- राज्य वातावरण की सुरक्षा और विकास करने के लिए देश के वन तथा वन्य जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा।
प्रश्न 22.
कोई ऐसे पाँच निदेशक सिद्धान्त बताएँ जिनका सम्बन्ध कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है?
उत्तर:
(1) राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि राज्य के सभी नागरिकों, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों,
(2) बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा अंगहीन होने की अवस्था में ओर से आर्थिक सहायता पाने का अधिकार हो,
(3) राज्य काम करने वालों के लिए न्यायपूर्ण मानवीय परिस्थितियों में काम करने की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा और स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता देने का प्रबन्ध करेगा,
(4) संविधान के लागू होने से दस वर्ष के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करेगा,
(5) राज्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करेगा।
प्रश्न 23.
राज्य-नीति के नीति निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कौन-सी शक्ति कार्य कर रही है?
उत्तर:
राज्य-नीति के नीति निदेशक सिद्धान्त न्यायसंगत नहीं हैं अर्थात् इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है, परन्तु इन सिद्धान्तों के पीछे जनमत (Public Opinion) की शक्ति है। लोकतन्त्र में जनमत का बहुत महत्त्व होता है और कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना करके अधिक समय तक पद पर बनी नहीं रह सकती।
चूँकि ये सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायता करते हैं, अतः कोई भी सरकार अपनी नीति का निर्माण करते समय इन्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं कर सकती। इनकी अवहेलना करने वाली सरकार के लिए अगले चुनावों में जीतने की सम्भावना नहीं होती। अतः निदेशक सिद्धान्तों के पीछे जनमत की शक्ति है।
प्रश्न 24.
भारतीय संविधान में दिए गए निदेशक सिद्धान्तों में से कोई पाँच सिद्धान्त लिखें।
उत्तर:
भारतीय संविधान में दिए गए पाँच निदेशक सिद्धान्त इस प्रकार हैं-
- राज्य ऐसे समाज का निर्माण करेगा, जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा,
- स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका कमाने के समान अवसर दिए जाएँगे,
- देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून तथा समान न्याय संहिता की व्यवस्था होनी चाहिए,
- बच्चों और नवयुवकों की नैतिक पतन तथा आर्थिक शोषण से रक्षा हो,
- राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा।
प्रश्न 25.
नीति निदेशक सिद्धान्त भारत में किस प्रकार एक धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी समाज की नींव डालते हैं?
उत्तर:
नीति निदेशक सिद्धान्त धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी समाज की आधारशिला रखते हैं। निदेशक सिद्धान्त राज्य सरकार को भारत में एक समान व्यवहार संहिता लागू करने का निर्देश देते हैं। निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा।
प्रश्न 26.
भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित निदेशक सिद्धान्त लिखें। अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन करें।
उत्तर:
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नीति से भी सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य-
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा,
- राष्ट्रों के मध्य उचित व सम्मानपूर्वक सम्बन्ध बनाए रखेगा,
- अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व कानूनों को सम्मान देगा,
- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने का प्रयास करेगा।
प्रश्न 27.
किन बातों के आधार पर राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की आलोचना की गई है?
उत्तर:
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की आलोचना दी गई बातों के आधार पर की गई है
- राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त न्याय-संगत नहीं हैं,
- राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में उचित वर्गीकरण तथा स्पष्टता का अभाव है,
- निदेशक सिद्धान्त केवल आश्वासन मात्र हैं,
- राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त अव्यावहारिक हैं,
- निदेशक सिद्धान्तों में स्थायित्व की कमी है।
प्रश्न 28.
मौलिक अधिकारों तथा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में कोई पाँच अन्तर बताएँ।
उत्तर:
मौलिक अधिकारों तथा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में अन्तर इस प्रकार हैं-
- मौलिक अधिकार न्याय-योग्य हैं, जबकि राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त न्याय-योग्य नहीं हैं,
- मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है, जबकि निदेशक सिद्धान्त अधिकतर सकारात्मक हैं,
- मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जबकि निदेशक सिद्धान्त सरकार के लिए हैं,
- मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतन्त्र का आधार हैं, जबकि निदेशक सिद्धान्त सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना में सहायक हैं,
- मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, जबकि निदेशक सिद्धान्तों को स्थगित नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 29.
मौलिक अधिकारों व राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों में टकराव की स्थिति में प्राथमिकता का क्या प्रश्न है?
उत्तर:
संविधान में स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में दिया है। सर्वप्रथम चम्पाकम दोराय राजन बनाम चेन्नई राज्य, 1951 के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों में वाद-योग्य होने के कारण माना कि यदि मौलिक अधिकारों व राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों में टकराव पाया जाता है तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गलती को महसूस किया और इनरी केरल एजुकेशन विधेयक, चन्द्रभवन बोर्डिंग केस, विजय कॉटन मिल्स केस इत्यादि अनेक मामलों में दोनों को समान धरातल पर माना और निदेशक तत्त्वों को मौलिक अधिकारों पर युक्ति-युक्त प्रतिबन्ध के रूप में स्वीकार किया।
संसद ने सन् 1971 में संविधान के 25वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 (b) व (c) में निहित निदेशक तत्त्वों की अनुच्छेद 14, 19 व 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित की। इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती केस, सन् 1973 में संविधान के मूलभूत ढाँचे के अन्तर्गत नहीं माना, लेकिन इसके बाद सन् 1976 में संसद ने जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी नीति-निदेशक तत्त्वों की अनुच्छेद 14, 19 व 31 में निहित समानता, स्वतन्त्रता व सम्पत्ति के मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित की तो सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में इस संशोधन को संविधान के मूलभूत ढाँचे के विरुद्ध मानते हुए अवैध घोषित कर दिया और प्रतिपादित किया कि संविधान का मूलभूत ढाँचा मौलिक अधिकारों व नीति-निदेशक तत्त्वों के मध्य सन्तुलन पर आधारित है।
दोनों एक-दूसरे के पूरक व सम्पूरक हैं। दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता देना संविधान के मूलभूत ढाँचे को विकृत तथा नष्ट करना होगा। … इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को समान माना है जिसमें केवल एक अपवाद अनुच्छेद 39 (b) व (c) की अनुच्छेद 14 व 19 में निहित समानता व स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता है, क्योंकि अनुच्छेद 31 को सन् 1978 के 44वें समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार मौलिक अधिकार और राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त एक-दूसरे के पूरक हैं।

प्रश्न 30.
राष्ट्रीय आपात का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पर नोट लिखिए।
उत्तर:
भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रीय आपात् का भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि जब देश पर किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण हुआ हो या आक्रमण होने की सम्भावना हो या देश में सशस्त्र विद्रोह फैल गया हो या ऐसा विद्रोह फैलने की सम्भावना हो तो वह देश में राष्ट्रीय आपात् की घोषणा कर सकता है।
राष्ट्रीय आपात् काल की घोषणा करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। यहाँ तक कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है। नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में भी शरण नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है, जैसा कि सन् 1975 में आपातकालीन घोषणा के बाद प्रशासन ने मनमाने तरीके से शक्ति का प्रयोग किया। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का स्थगित किया जाना प्रजातन्त्र की भावना के विपरीत है।
निबंधात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
प्रो० लास्की के अनुसार, “मूल अधिकार जीवन की उन आवश्यक अवस्थाओं को कहते हैं, जिनके बिना व्यक्ति के जीवन का विकास असम्भव है।” (Rights are those conditions of Social Life without which no man can seek in general, to be himself at his best.), अर्थात् प्रो० लास्की के अनुसार ये आवश्यक अवस्थाएँ व्यक्ति के चरित्र के विकास के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि व्यक्ति और राज्य की उन्नति एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है,
अतः अधिकार एक प्रकार से राज्य के विकास और उन्नति के लिए भी अनिवार्य हैं। लगभग सभी राज्य अपने नागरिकों के लिए इन आवश्यक अवस्थाओं अथवा सुविधाओं की संविधान में व्यवस्था करते हैं। इंग्लैण्ड जैसे अलिखित संविधान में मौलिक अधिकार अलिखित हैं, परन्तु अमेरिका जैसे राज्यों में, जहां लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार लिखित संविधान का भाग हैं।
भारतीय संविधान लिखित संविधान है, अतः भारत में मूल अधिकार लिखित संविधान का भाग हैं। संविधान के तीसरे भाग के 12 से 35 अनुच्छेदों में मूल अधिकार दिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकार केवल लिखित ही नहीं, बल्कि न्याय-योग्य भी हैं। मौलिक अधिकारों को न्याय-योग्य इसलिए ठहराया गया है कि विधानमण्डल और कार्यकारिणी के सदस्य नागरिकों को सताने न लगें।
कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका पर लोगों के अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व है अर्थात् न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न होने पाए, अतएव न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वह विधानमण्डल द्वारा बनाए गए उन सब कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन् करते हैं। मौलिक अधिकारों के तत्त्व या विशेषताएँ (Characteristics or Features of Fundamental Rights)-मौलिक अधिकारों के कुछ विशेष तत्त्व निम्नलिखित हैं
1. मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं (Fundamental Rights are Justiciable):
मौलिक अधिकार केवल नाममात्र के ही नहीं हैं, बल्कि इनको अदालत के द्वारा संरक्षित किया गया है। यदि किसी मनुष्य का अधिकार सरकार द्वारा या किसी और द्वारा छीना जाए तो वह अदालत की शरण ले सकता है और उसको न्याय मिलेगा। हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे ही उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
2. मौलिक अधिकार सीमित हैं (Fundamental Rights are Limited):
ये मौलिक अधिकार सीमित हैं। नागरिक इनका प्रयोग मनमानी से नहीं कर सकता। इनके ऊपर उचित प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं। सुरक्षा, शान्ति बनाए रखने के लिए इन पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।
3. अति विस्तृत (Most Elaborate):
संविधान के तृतीय भाग में 24 अनुच्छेद (अनुच्छेद 12 से 35) नागरिक के मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 में ऐसे साधारण उपबन्ध हैं, जिनका सम्बन्ध सभी अधिकारों से है। अनुच्छेद 14 से 30 और अनुच्छेद 32 में नागरिकों को छः प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक रूप में अनुच्छेद 31 द्वारा नागरिकों को ‘सम्पत्ति का अधिकार’ दिया गया था, परन्तु 44वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान में से निकाल दिया गया है।
4. मौलिक अधिकार निलम्बित किए जा सकते हैं (Fundamental Rights can be Suspended):
अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 द्वारा राष्ट्रपति को आपात्काल की स्थिति की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति आपात्काल की घोषणा. द्वारा इन अधिकारों को निलम्बित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32 में वर्णित सवैधानिक उपचारों के अधिकार पर भी राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में प्रतिबन्ध लगा सकता है।
यहाँ यह वर्णन करने योग्य है कि नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी आपात्कालीन अवस्था में भी नागरिकों के अदालत में शरण लेने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई है।
5. संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है (Parliament can Curtail the Fundamental Rights):
संसद मौलिक अधिकारों में हर प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। यह व्यवस्था 1971 में 24वें संशोधन द्वारा संविधान में की गई थी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भी यह व्यवस्था की गई है कि संसद मौलिक अधिकारों वाले प्रकरण सहित सम्पूर्ण संविधान में परिवर्तन कर सकती है तथा संसद द्वारा किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका अभिप्रायः यह हुआ कि संसद संविधान संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या सीमित कर सकती है।
6. सकारात्मक व नकारात्मक प्रकृति (Positive and Negative Nature):
मौलिक अधिकारों की सकारात्मक प्रकृति से तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ कार्य करने का अधिकार प्रदान करते हैं और नकारात्मक प्रकृति से अर्थ है कि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।
भारतीय मौलिक अधिकारों में ये दोनों ही प्रवृतियाँ पाई जाती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण समानता का अधिकार है, जिसमें नागरिकों को ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before Law) के साथ-साथ ‘कानून का समान संरक्षण’ (Equal Protection of Law) का अधिकार दिया गया है।
‘कानून के समक्ष समानता’ की प्रकृति नकारात्मक है, क्योंकि यह राज्य को नागरिकों में भेद-भाव करने से रोकती है और इसके विपरीत ‘कानून का समान संरक्षण’ की प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि इसके अन्तर्गत राज्य नागरिकों में भेद-भाव कर सकता है, ताकि गरीब व पिछड़े वर्गों का समान संरक्षण मिल सके।
7. मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं, प्राकृतिक अधिकार नहीं (Fundamental Rights are conferrred by the Constitution, not Natural Rights):
भारत में केवल वे ही मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अमेरिका की भाँति भारत में भी प्राकृतिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। न्यायपालिका का संरक्षण संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को ही प्राप्त है।
8. भारतीय पृष्ठभूमि (Indian Background):
भारत में मौलिक अधिकार किसी अन्य देश की नकल नहीं हैं, बल्कि विशिष्ट भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार प्रदान किए गए हैं, जैसे छुआछूत का निषेध । छुआछूत भारतीय समाज में ही पाया जाता था, इसलिए इसका निषेध एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार भारतीय समाज के बहुधर्मी रूप को देखते हुए दिया गया है।
9. सभी पर लागू होते हैं (Binding upon Everybody):
मौलिक अधिकार राज्य की सभी संस्थाओं, जिनमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकारी संस्थाएँ और यहाँ तक कि भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी इनको मानने से इन्कार नहीं कर सकता और न ही किसी को इनके उल्लंघन का अधिकार है।
10. मुख्यतया राजनीतिक प्रकृति के (Primarily of Political Nature):
भारत में मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक प्रकृति के हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकार राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों में दिए गए हैं। संविधान सभा का विचार था कि चूंकि अभी भारत के पास इतने अधिक साधन नहीं हैं कि नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक अधिकार भी सुलभ कराए जा सकें। अतः राजनीतिक अधिकार ही प्रदान कर दिए गए, ताकि राजनीतिक दृष्टि से लोकतन्त्र स्थापित किया जा सके।
11. नागरिक व व्यक्ति में अन्तर किया गया है (Difference between Citizen and People):
भारत में कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं तो कुछ अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं। व्यक्तियों को दिए गए अधिकार नागरिकों व विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, जब कि नागरिकों को दिए गए अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। उदाहरणार्थ, स्वतन्त्रता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। समानता का अधिकार यदि नागरिकों को प्राप्त है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है।
12. केन्द्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध (Limitations on the Powers of the Centre and the State Governments):
मौलिक अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को मौलिक अधिकारों के अनुसार ही कानून बनाने पड़ते हैं और ये सरकारें कोई ऐसा कानून नहीं बना सकतीं जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति के विरुद्ध हो। यदि ये सरकारें मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बना दें तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है।
प्रश्न 2.
भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उन पर लगी सीमाओं सहित विवेचन कीजिए।
अथवा
हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर एक लेख लिखिए।
अथवा
निम्नलिखित पर नोट लिखिए
(1) समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक,
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक,
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक,
(4) संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक।
उत्तर:
सन् 1979 से पहले भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परन्तु इसके पश्चात् इन अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। 30 अप्रैल, 1979 को 44वाँ संविधान संशोधन राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस संशोधन के अन्तर्गत नागरिकों का ‘सम्पत्ति का अधिकार’ (Right to Property) मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया और अब यह अधिकार एक साधारण अधिकार (Ordinary Right) बन गया है। 44वें संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी यह व्यवस्था 19 जून, 1979 को लागू की गई थी। भारतीयों के शेष छः अधिकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन निम्नलिखित है
1. समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक [Right to Equality, Articles 14 to 18|-अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित अधिकारों द्वारा भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के अधिकार के कई पक्ष हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है
(i) कानून के सामने समानता (Equality before Law):
अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। कानून की दुनिया में ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, रंग या नस्ल, जाति, जन्म, धर्म आदि के आधार पर कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण नागरिक तक सभी कानून की दृष्टि में समान समझे जाते हैं तथा कानून समान रूप से ही सबकी रक्षा करता है।
(ii) कोई भेदभाव नहीं (No Discrimination) संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, जैसे होटल, तालाब, कुएँ, सिनेमा घर, दुकानों आदि, के प्रयोग के लिए किसी को मनाही नहीं होगी। अपवाद (Exceptions) अनुच्छेद 15 के दो अपवाद हैं-(क) राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान कर सकता है, (ख) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रकार की व्यवस्था कर सकता है।
(iii) अवसर की समानता (Equality of Opportunity):
अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी। नियुक्ति करते समय सरकार किसी व्यक्ति के साथ रंग, नस्ल, जाति, जन्म, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। किसी व्यक्ति को इन बातों के आधार पर उसके पद से पदच्युत नहीं किया जा सकता, परन्तु सरकार को संविधान की ओर से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की छूट है।
अपवाद (Exceptions) इस व्यवस्था के तीन अपवाद हैं-प्रथम, कुछ विशेष पदों के लिए निवास स्थान सम्बन्धी आवश्यक शर्ते लगाई जा सकती हैं। द्वितीय, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तृतीय, किसी धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक संस्था से सम्बन्धित पदों पर एक विशेष धर्म अथवा सम्प्रदाय के लोगों की नियुक्ति की जा सकती है।।
(iv) अस्पृश्यता का अन्त (Abolition of Untouchability):
अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है। जो व्यक्ति अस्पृश्यता को किसी भी तरीके से लागू करने का यत्न करता है, अथवा प्रोत्साहित करता है उसको कानून द्वारा दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी सार्वजनिक स्थान मन्दिर, होटल, कुएँ, स्कूल, कॉलेज आदि हरिजन लोगों के लिए खुले हैं। उनको इनके प्रयोग से रोकना कानूनी अपराध है।
(v) उपाधियों की समाप्ति (Abolition of Titles):
अंग्रेज़ सरकार भारत में नागरिकों को कई प्रकार की उपाधियाँ प्रदान करती थी। ये उपाधियाँ हमारे भारतीय समाज में भेदभाव की भावना पैदा करती थीं। ऐसी स्थिति की समाप्ति के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा शैक्षणिक अथवा सैनिक उपाधियों के अलावा राज्य को अन्य किसी प्रकार की उपाधियाँ देना वर्जित किया गया है।
2. स्वतन्त्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक (Right to Freedom,Articles 19 to 22):
संविधान में स्वतन्त्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। यह अधिकार ‘मौलिक अधिकारों की आत्मा’ है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य अधिकारों का कोई महत्त्व नहीं रहता। इस अधिकार के आधार पर ही प्रजातन्त्रीय समाज की कल्पना की जा सकती है। इस विषय में पायली महोदय का कथन महत्त्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा है, “संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल करके ठीक ही किया है तथा इस प्रकार प्रजातन्त्रीय समाज के विकास में सहायता की है।”
(1) अनुच्छेद 19 के द्वारा निम्नलिखित स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं…
(क) भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता,
(ख) शान्तिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता,
(ग) संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता,
(घ) भारत के किसी भी क्षेत्र में आने-जाने की स्वतन्त्रता,
(ङ) भारत के किसी भाग में रहने या निवास करने की स्वतन्त्रता,
(च) कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतन्त्रता।
इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है
(क) भाषण एवं लेखन की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech and Expression)-सभी नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। वे बोलकर या लिखकर और छपवाकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लोकतन्त्र में इस अधिकार का बड़ा महत्त्व होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति हो सकती है।
परन्तु इस अधिकार पर राज्य न्यायालय के अपमान, सदाचार तथा नैतिकता, राज्य की सुरक्षा आदि के आधार पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। कोई भी नागरिक इस अधिकार का प्रयोग दूसरे का अपमान करने के लिए नहीं कर सकता।
(ख) शान्तिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता (Freedom to Assemble Peacefully and without Arms) नागरिकों को बिना हथियार और शान्तिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने, सभा करने तथा जुलूस निकालने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। इन सभाओं और जुलूसों में नागरिक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयत्न कर सकते हैं।
इस स्वतन्त्रता पर भी राज्य उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। सार्वजनिक शांति और व्यवस्था, भारत की अखण्डता व सुरक्षा की दृष्टि से इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 144 का लगाया जाना इसी प्रतिबन्ध का एक उदाहरण है।
(ग) संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता (Freedom to form Associations and Unions)-नागरिकों को अपने विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने और संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता दी गई है। इन संघों और समुदायों को भी अपना कार्य स्वतन्त्रता-पूर्वक करने का अधिकार है। परन्तु कोई समुदाय या संघ ऐसा कार्य नहीं कर सकता, जिससे देश की अखण्डता व सुरक्षा को खतरा पैदा हो, जो अनैतिक हो अथवा शान्ति व व्यवस्था में बाधक बने।
(घ) भारत के किसी भी क्षेत्र में आने-जाने की स्वतन्त्रता (Freedom to Move freely Throughout the Territory of India)- सभी नागरिकों को भारत के समस्त क्षेत्र में घूमने-फिरने और आने-जाने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने के लिए किसी भी तरह का आज्ञा-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।
नागरिक भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना रोक-टोक के आ-जा सकते हैं, परन्तु इस स्वतन्त्रता पर भी सार्वजनिक शांति, सुरक्षा, व्यवस्था तथा अनुसूचित कबीलों के हितों की दृष्टि से उचित सीमा लगाई जा सकती है और नागरिकों के घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाए जाते रहे हैं।
(ङ) भारत के किसी भाग में रहने और निवास करने की स्वतन्त्रता (Freedom to Reside and Settle in any part of the Territory of India)-भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतन्त्रता दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रहने और निवास करने पर कोई अंकुश नहीं है, नागरिक जहाँ उचित समझे रह सकता है, परन्तु राज्य इस पर भी उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।
(च) कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतन्त्रता (Freedom to practise any Profession or carry on any Occupation, Trade or Business)- सरकार किसी नागरिक को कोई कार्य विशेष करने या न करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अपनी आजीविका कमाने के लिए नागरिकों को कोई भी व्यवसाय, पेशा या व्यापार करने की स्वतन्त्रता है, जिसे वे उचित समझें।
इस स्वतन्त्रता पर भी उचित प्रतिबन्ध है। सरकार जन-हित में किसी भी व्यापार, काम-धन्धे और व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगा सकती है और अनैतिक व्यापार को रोक सकती है। सरकार किसी व्यवसाय के लिए व्यावसायिक योग्यताएँ भी निश्चित कर सकती है, जैसे चिकित्सा, व्यवसाय, वकालत आदि के लिए योग्यताएँ। सरकार कानून द्वारा किसी भी व्यापार को अपने स्वामित्व में ले सकती है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी स्वतन्त्रताओं को असीमित रूप में नहीं दिया गया, बल्कि उन पर उचित प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और लगाए जा सकते हैं। अधिकतर सार्वजनिक शांति और व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा और अखण्डता, सार्वजनिक नैतिकता, लोक-हित, अनुसूचित जातियों और कबीलों के हितों आदि के आधार पर ही ये प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और लगाए जा सकते हैं। जब नगर में अशांति हो तो कयूं भी लगाया जाता है और घर से निकलने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
(2) अनुच्छेद 20 के अनुसार-
(क) व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दण्ड नहीं दिया जा सकता जो उसके अपराध करते समय लागू नहीं था।
(ख) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध की एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।
(ग) किसी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
(3) अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 44वें संशोधन द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि नागरिकों के इस अधिकार को आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका भाव यह हुआ कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान अन्य स्वतन्त्रताएँ तो समाप्त की जा सकती हैं, परन्तु नागरिकों की ‘जीवन या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ को ऐसी स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
(4) अनुच्छेद 22 विशेष रूप से बन्दियों के अधिकारों की घोषणा करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार,
(क) किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध से अवगत कराए बिना बन्दी नहीं बनाया जा सकता।
(ख) अपराधी को उसकी इच्छानुसार किसी वकील से परामर्श लेने की छूट है।
(ग) अपराधी को गिरफ्तार करने के 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर किसी निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।
(घ) न्यायालय की अनुमति के बिना किसी दोषी को 24 घण्टे से अधिक बन्दी नहीं रखा जा सकता।
अपवाद इस अधिकार के निम्नलिखित अपवाद भी हैं-
(क) ये अधिकार शत्रु-देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे,
(ख) निवारक नजरबन्दी (Preventive Detention) के अधीन की गई गिरफ्तारी के सन्दर्भ में उपर्युक्त व्यवस्थाएँ लागू नहीं होंगी, निवारक नजरबन्दी के सम्बन्ध में 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्थाएँ की गई हैं कि-
(क) नजरबन्दी का मामला दो महीने के अन्दर सलाहकार मण्डल (Advisory Board) के पास जाना आवश्यक है,
(ख) सलाहकार मण्डल का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा,
(ग) सलाहकार मण्डल का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा, लेकिन उसके अन्य सदस्य वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं,
(घ) नजरबन्द किए गए व्यक्ति को शीघ्र-से-शीघ्र उसकी नजरबन्दी का कारण बताया जाएगा।
उपर्युक्त व्यवस्थाएँ 1975-77 की आपात स्थिति के कटु अनुभवों को ध्यान में रखकर ही की गई थीं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत बनाया गया है। आलोचना (Criticism)-स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार की निम्नलिखित अनुच्छेदों पर आलोचना की जाती है
(क) नागरिकों की स्वतन्त्रताओं पर अनेक सीमाएँ लगा दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य-सत्ता के सम उपर्युक्त स्वतन्त्रताएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। ये स्वतन्त्रताएं यदि एक हाथ से दी गई हैं तो दूसरे हाथ से छीन ली गई हैं।
(ख) सीमाएँ अत्यधिक व्यापक होने के कारण अस्पष्टता से ग्रसित हो जाती हैं। परिणामस्वरूप विधायिका व न्यायपालिका में टकराव की सम्भावना बनी रहती है।
(ग) निवारक नजरबन्दी का अधिकार राज्य को प्राप्त है जिसके कारण शान्ति काल में भी जीवन तथा निजी स्वतन्त्रता का अधिकार अर्थहीन हो जाता है। न्यायाधीश मुखर्जी के शब्दों में, “जहाँ तक मुझे मालूम है संसार के किसी भी देश में निवारक नज़रबन्दी को संविधान का अटूट भाग नहीं बनाया गया है, जैसा कि भारत में किया गया है, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।”
यद्यपि. उपर्युक्त आलोचनाएँ सही हैं और लोकतन्त्र पर प्रश्न-चिह्न लगाती हैं, नागरिक स्वतन्त्रताओं को दुष्प्रभावित करती हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारतीय गणराज्य का जन्म साम्प्रदायिक हिंसा, हत्या तथा लूट-पाट के वातावरण में हुआ है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए प्राथमिक अनिवार्यता राष्ट्र व गणराज्य की राष्ट्र-विरोधी असामाजिक तत्त्वों से सुरक्षा है।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक (RightAgainst Exploitation,Articles 23 to 24)-शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य है-समाज के निर्बल वर्गों को शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से बचाना। इस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हैं
(1) मनुष्यों के क्रय-विक्रय और उनके शोषण पर प्रतिबन्ध (Prohibition of Sale and Purchase of Human beings and their Exploitation): हजारों वर्ष गुलाम रहने के बाद भारतीय समाज में बहुत-सी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थीं जिनमें से एक थी-स्त्रियों व बच्चों का क्रय-विक्रय। मनुष्यों का पशुओं के समान क्रय-विक्रय किया जाता था और उन्हें दास बनाकर मनमाने तरीके से उनका प्रयोग किया जाता था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 23 के अनुसार, मानव के इस शोषण के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाया है और इस प्रकार अब भारत में स्त्रियों, पुरुषों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस व्यवस्था का उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया है।
(2) बेगार लेने पर प्रतिबन्ध (Prohibition on Forced Labour)-भारत के मध्य काल में जमींदार लोग तथा राजा और नवाब अपने अधीनस्थ लोगों से बेगार लेते थे। अपने निजी कार्य उनसे कराकर उनके बदले में उन्हें कुछ नहीं देते थे, परन्तु अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी से बेगार नहीं ले सकता अर्थात् बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं लिया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विपरीत कोई काम कराया जा सकता है। अब ये दोनों ही बातें एक दण्डनीय अपराध घोषित हो चुकी हैं।
अपवाद (Exceptions)-संविधान के अनुच्छेद 23 में दिए गए अधिकारों पर एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और वह यह है कि सरकार को जनता के हितों के लिए अपने नागरिकों से आवश्यक सेवा करवाने का अधिकार है। उदाहरणस्वरूप, सरकार नागरिकों को अनिवार्य सैनिक-सेवा तथा अनिवार्य सामाजिक सेवा करने के लिए कानून बना सकती है, परन्तु ऐसा करते हुए सरकार धर्म, वंश, जाति, वर्ग अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती।
(3) कारखानों आदि में छोटी आयु के बच्चों को काम करने की मनाही (Prohibition of Employment of Children in Factories etc.)-कारखानों व खानों के मालिक छोटी आयु के बच्चों को काम पर लगाना अति लाभदायक समझते थे क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती थी, परन्तु अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खानों में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना अब एक दण्डनीय अपराध है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
4. साँस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक (Cultural and Educational Rights, Articles 29 to 30)
(1)अनुच्छेद 29 तथा 30 के अन्तर्गत नागरिकों को, विशेषतया अल्पसंख्यकों को, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार निम्नलिखित हैं अनुच्छेद 29 के अनुसार, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग या उसके किसी भाग को, जिसकी अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति हो, यह अधिकार है कि वह अपने संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करे। अनुच्छेद 29 के अनुसार, केवल अल्पसंख्यकों को ही अपनी भाषा, संस्कृति इत्यादि को सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह अधिकार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को प्राप्त है।
(2) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा या उसकी सहायता से चलाई जाने वाली शिक्षा संस्था में प्रवेश देने से धर्म, जाति, वंश, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर इन्कार नहीं किया जा सकता। 1951 में मद्रास (चेन्नई) सरकार ने एक मैडिकल कॉलेज में सीटों का विभाजन भिन्न-भिन्न जातियों के आधार पर कर दिया था जिसके कारण चम्पाकम नामक एक ब्राह्मण लड़की को उस कॉलेज में दाखिला न मिल सका, क्योंकि उस जाति को दिए गए
सभी स्थान पूर्ण हो गए थे। चम्पाकम ने अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए न्यायालय में रिट (Writ) की। उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
(3) अनुच्छेद 30 के अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें तथा उनका प्रबन्ध करें।
(4) अनुच्छेद 30 के अनुसार, राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय शिक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबन्ध के अधीन है, चाहे वे अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हों या धर्म के आधार पर। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 30 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित की गई व चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं की सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से लेने के लिए कानून का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि कानून के अन्तर्गत निर्धारित की गई रकम से अल्पसंख्यकों के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 29 तथा 30 द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत में इस अधिकार का बहुत महत्त्व है, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों तथा भाषाओं वाले लोग रहते हैं।

प्रश्न 3.
धार्मिक स्वतन्त्रता पर एक नोट लिखिए। अथवा भारतीय संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार की व्याख्या करें।
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित है
1. अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Conscience and Freedom to Profess and Propagate any Religion)-अनुच्छेद 25 के द्वारा सभी को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता है। इसका अभिप्रायः है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसी चाहे पूजा-पद्धति को अपना सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता है। राज्य किसी धर्म विशेष को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, परन्तु उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार, “छल, कपट, प्रलोभन या बल-प्रयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म-परिवर्तन कराना संविधान के विरुद्ध है।”
प्रतिबन्ध (Limitations) अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतन्त्रता पर जिस आधार पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं-
(1) यदि धर्म-प्रचार या धर्म-परिवर्तन लोक व्यवस्था, सदाचार और जन स्वास्थ्य के विरुद्ध है तो राज्य द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है,
(2) अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है,
(3) प्रचार के नाम पर धर्म-परिवर्तन की मनाही है,
(4) समाज सुधार एवं कल्याण के लिए विभिन्न धार्मिक परम्पराओं और अन्धविश्वासों को दूर किया जा सकता है अर्थात् धर्म के नाम पर सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता,
(5) हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों को सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है।
2. धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता (Freedom to Manage Religious Affairs):
संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित स्वतन्त्रताएँ हैं
- धार्मिक व लोकोपकारी संस्थाएँ चलाना,
- अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबन्ध करना,
- चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना,
- कानून के अनुसार उपर्युक्त सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।
धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सके। उदाहरणतः जून 1984 में ऑप्रेशन ब्लू स्टार के द्वारा स्वर्ण मन्दिर अमृतसर में सेना को इसलिए प्रवेश करना पड़ा था क्योंकि उसमें राष्ट्र-विरोधी असामाजिक तत्त्वों का जमाव हो चुका था।
3. किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए कर की अदायगी से छूट (Freedom from Payment of Taxes for Promotion of any Particular Religion) संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसको किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए व्यय किया जाना हो। राज्य कर के रूप में लिए गए धन को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए प्रयोग नहीं करेगा, परन्तु यदि राज्य बिना किसी भेदभाव के धार्मिक एवं अन्य संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद लागू नहीं होगा।
4. राजकीय शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध (No Religious Teachings in Educational Institutions maintained by State Funds) अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत उन राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जिनका सारा खर्च राज्य करता हो, लेकिन यह प्रतिबन्ध उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त है तथा आर्थिक सहायता भी मिलती है, लेकिन सारा खर्च राज्य न करता हो। किन्तु ऐसी शिक्षा संस्थाओं में भी किसी व्यक्ति को उसकी व उसके अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा प्रशासित तथा धर्मस्व व न्यास के अधीन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
इस प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना में घोषित उद्देश्यों-धर्म-निरपेक्षता व अंतःकरण की स्वतन्त्रता को निश्चित बनाता है जिसके अन्तर्गत राज्य का कोई सरकारी धर्म नहीं है और न ही राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकता है। धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार पर निम्नलिखित तीन सीमाएँ हैं
(1) राज्य शान्ति और व्यवस्था, नैतिकता तथा जन-स्वास्थ्य के आधार पर इस अधिकार पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। सती-प्रथा तथा देवदासी प्रथा पर रोक इसी आधार पर लगा दी गई है।
(2) धार्मिक समुदायों की आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने वाले कानून बनाए जा सकते हैं।
(3) हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। हिन्दू संस्थाओं के अन्तर्गत सिक्ख, जैन तथा बौद्ध समुदायों की संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
प्रश्न 4.
भारतीय संविधान में लिखित संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार का विवेचन कीजिए। अथवा संवैधानिक उपचार के अधिकार का विश्लेषण करें।
उत्तर:
सवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)-भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान में ही उन अधिकारों की रक्षा भी की गई है। मौ की रक्षा की इस व्यवस्था के अभाव में सरकार अथवा कोई अन्य नागरिक इन अधिकारों के उपयोग में बाधा पैदा कर सकता था और इस प्रकार ये मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए महत्त्वहीन हो जाते।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार यदि सरकार या कोई नागरिक मौलिक अधिकारों से किसी को वंचित करता है तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की में न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार-
- भारत के उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भिन्न-भिन्न आदेश जारी करने के अधिकार दिए गए हैं,
- उच्चतम न्यायालय को विभिन्न आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार है,
- संसद कानून बनाकर किसी भी न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश (writ) जारी करने की शक्ति दे सकती है,
- उन परिस्थितियों को छोड़कर, जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता।
इसीलिए डॉ० अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने इस अनुच्छेद के सन्दर्भ में लिखा था, “यदि मुझे कोई पूछे कि संविधान का कौन-सा महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान प्रभाव शून्य हो जाएगा तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान का हृदय है।” मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित आदेश जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है
(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus):
लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है-‘हमें शरीर दो’ (Let us have the body), अर्थात् शरीर हमारे सामने पेश करो। इस आदेश के अन्तर्गत न्यायपालिका को अधिकार है कि वह सरकार को बन्दी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है।
ऐसे लेख का प्रार्थना-पत्र बन्दी स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकता है, यदि वह महसूस करे कि उसे गैर-कानूनी ढंग से बन्दी बनाया गया है।
बन्दी जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत होता है तो न्यायालय उसके मामले पर विचार करता है और यदि न्यायालय यह समझे कि बन्दी को वास्तव में ही गैर-कानूनी ढंग से बन्दी रखा गया है तो वह उसके मुक्त किए जाने का आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार पुलिस किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बन्दी नहीं बनाए रख सकती। इस अधिकार को आपातकाल में भी निलम्बित नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ने इस अधिकार का प्रयोग करके नागरिकों को पुलिस के अत्याचार से बचाया है। राजनीतिक कैदियों को भी कई बार न्यायालय ने इसका प्रयोग करके मुक्त किया है। इस प्रकार यह लेख नागरिक की दैहिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण साबित हुआ है।
(2) परमादेश लेख (Writ of Mandamus):
इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी या संस्था को अपना कर्त्तव्य-पालन करने के आदेश दे सकता है। लैटिन भाषा के इन शब्दों का अर्थ है “हम आदेश देते हैं” (We Command)। यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करे कि कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो वह न्यायालय को ऐसा आदेश जारी करने का प्रार्थना-पत्र दे सकता है।
इस प्रार्थना पर विचार करने के बाद न्यायालय यदि यह अनुभव करे कि वास्तव में ही उस अधिकारी या संस्था द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं हो रहा है तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है और उस आदेश को मानना उस अधिकारी या संस्था का कर्तव्य है।
(3) प्रतिषेध लेख (Writ of Prohibition):
इस आदेश या लेख का अर्थ है-‘रोकना’ या ‘मनाही करना’ । यदि कोई कर्मचारी या संस्थान कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जिसका उसे अधिकार नहीं है और इससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता हो तो वह व्यक्ति न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे सकता है और यदि न्यायालय यह अनुभव करे कि कर्मचारी या अधिकारी या संस्था अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जा रहा है या कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध जा रहा है तो वह प्रतिषेध लेख जारी करके उसे ऐसा करने से रोक सकता है।
(4) अधिकार पृच्छा लेख (Writ of Quo-Warranto):
इन शब्दों का अर्थ है-“किस अधिकार से” (Under What Authority)। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने का दावा करता है, जिसे करने का उसे अधिकार नहीं या किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध कोई पद-ग्रहण कर लिया हो या किसी के पास पद की योग्यता न हो तो कोई भी नागरिक न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर उसे ऐसा करने से रोकने की प्रार्थना कर सकता है।
न्यायालय यह आदेश जारी करके उस अधिकारी या कर्मचारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कह सकता है और यदि वह गैर-कानूनी ढंग से पद ग्रहण किए हुए है तो उसे पदच्युत भी कर सकता है।
(5) उत्प्रेषण लेख (Writof Certiorari):
इसका अर्थ है-“पूर्णतः सूचित करो।” (Be More Fully Informed)। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को दिया जाता है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय में चल रहे किसी भी मुकद्दमे का पूर्ण ब्यौरा तथा रिकार्ड अपने पास मॅगवा सकता है और यदि उच्च न्यायालय अनुभव करे कि निम्न न्यायालय ने अपने अधि का उल्लंघन किया है
या कानन की प्रक्रिया का समचित पालन नहीं किया है तो वह उस मकद्दमे को स्वयं भी सन सकता है और उसे कुछ निर्देश सहित निम्न न्यायालय को वापस भेज सकता है। इसके द्वारा नागरिकों को न्यायपालिका के अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था की गई है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। प्रभावित व्यक्ति, अर्थात् जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति तथा संस्थाएँ भी इन उपचारों का प्रयोग कर सकते हैं। न्यायपालिका ने लोगों द्वारा लिखे गए साधारण पत्रों, समाचार-पत्रों में छपी खबरों आदि को भी प्रार्थना-पत्र (Writ Petition) मानकर कार्रवाई की है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया है जो कि अत्यन्त सराहनीय है।
निष्कर्ष (Conclusion)-निःसन्देह भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कई पक्षों से आलोचना की गई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मौलिक अधिकारों के अध्याय में सामाजिक और आर्थिक अधिकार सम्मिलित न करना एक बहुत बड़ी भूल है और इससे मौलिक अधिकार खोखले बनकर रह गए हैं। इन अधिकारों की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि सरकार को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्तियाँ बहुत दी गई हैं, परन्तु इन सब बातों के बावजूद भी हमें मानना पड़ता है कि मौलिक अधिकार लोकतन्त्र की नींव हैं। अधिकार कभी असीमित नहीं होते।
संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ मूल अधिकारों पर बन्धन न लगाए गए हों। मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की गई है और कार्यपालिका और संसद की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा दिया गया है। हम एम०वी० पायली (M.V. Paylee) के इस कथन से ‘सहमत हैं, “सम्पूर्ण दृष्टि में संविधान में अंकित मौलिक अधिकार भारतीय प्रजातन्त्र को दृढ़ तथा जीवित रखने का अधिकार हैं।”
प्रश्न 5.
किन अनुच्छेदों पर मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई है? व्याख्या करें। अथवा भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की आलोचना किन-किन आधारों पर की जाती है?
उत्तर:
हमारे संविधान-निर्माताओं ने भारत को प्रभुतासम्पन्न प्रजातन्त्रीय गणराज्य घोषित किया है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप ही भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यवस्था में कछ दोष पाए जाते हैं। विद्वानों ने इन दोषों को देखते हए यहाँ तक कह दिया है कि मौलिक अधिकार नामक भाग को ‘मौलिक अधिकार तथा उनकी सीमाएँ’ नाम दे दिया जाए। मौलिक अधिकारों की अग्रलिखित अनुच्छेदों पर आलोचना की गई है
1. आर्थिक अधिकारों का न होना (Omission of Economic Rights):
आलोचकों का कहना है कि यद्यपि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है, परन्तु इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों, जैसे कार्य पाने का अधिकार (Right to Work), ‘आराम तथा विश्राम का अधिकार’, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार (Right to Social Securities) भारतीयों को प्रदान नहीं किए गए। साम्यवादी देशों; जैसे रूस आदि में इन अधिकारों को प्रमुख स्थान दिया गया है।
2. भारतीयों को केवल वे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान में दिए गए हैं (Only Enumerated Rights are granted to Indians):
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि भारतीय नागरिकों को केवल वही अधिकार दिए गए हैं, जिनका कि संविधान में उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, परन्तु अमेरिका के नागरिकों को संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा वे अधिकार भी प्राप्त हैं, जो साधारण कानून (Common Law) तथा प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) पर आधारित हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
3. मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्धों का होना (Limitations on Fundamental Rights):
मौलिक अधिकारों की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार देकर उन पर प्रतिबन्धों तथा अपवादों का घेरा लगाकर दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। इस व्यवस्था से मौलिक अधिकारों की वास्तविकता ही समाप्त हो जाती है।
परन्तु यह आलोचना पूरी तरह से ठीक नहीं है। कोई भी मौलिक अधिकार असीमित नहीं हो सकता तथा देश की बदलती हई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन भी करना पड़ता है। इस व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों के बारे में अन्तिम सत्ता संसद के हाथों में होनी चाहिए। यही व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई है।
4. निवारक नजरबन्दी व्यवस्था (Preventive Detention Provision):
अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही संविधान में निवारक नजरबन्दी की भी व्यवस्था की गई है। जिन व्यक्तियों को निवारक नज़रबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हो, उनको अनुच्छेद 22 में दिए गए अधिकार प्राप्त नहीं होते। निवारक नज़रबन्दी के अधीन सरकार कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकद्दमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में बन्द कर सकती है तथा उसकी स्वतन्त्रता का हनन कर सकती है।
5. मौलिक अधिकारों पर संसद का नियन्त्रण (Control of Parliament Over Fundamental Rights):
भारतीय संविधान के अनुसार, कानून द्वारा निर्धारित ढंग (Procedure Established by Law) की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार मौलिक अधिकारों के बारे में अन्तिम निर्णय संसद के हाथों में है।
संसद जो भी कानून बनाती है, यदि वह संविधान के अनुकूल है, तो उच्चतम न्यायालय उसे वैध मानेगा। इस व्यवस्था की बजाय ‘उचित कानूनी प्रक्रिया’ (Due Process of Law) को अपनाया जाना चाहिए था, जिससे कि मौलिक अधिकारों के बारे में अन्तिम सत्ता उच्चतम न्यायालय के हाथों में होती, परन्तु भारत में कानून द्वारा निर्धारित ढंग अपनाने का मुख्य कारण मुकद्दमेबाजी को कम करना था।
6. न्यायपालिका के निर्णय संसद के कानूनों द्वारा निरस्त (Decisions of Judiciary struck by Parliament):
उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार संसद के कानूनों को इस आधार पर निरस्त किया है कि वे कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, परन्तु संसद ने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका द्वारा निरस्त घोषित किए गए कानूनों को वैध तथा सवैधानिक घोषित कर दिया।
7. कठिन भाषा (Difficult Language):
सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) के अनुसार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख बहुत कठिन भाषा में किया गया है। इसको साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। उनका कहना है कि भारतीय मौलिक अधिकारों की भाषा अमेरिका के संविधान की तरह सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए थी।
8. न्याय का महँगा होना (Costly Judicial Remedies):
भारत में न्याय-व्यवस्था वैसे ही महँगी है। इधर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति या तो उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे। इसका अर्थ है-बहुत अधिक धन खर्च करना, जो कि साधारण नागरिक के लिए असहनीय है। न्याय-व्यवस्था सरल तथा सस्ती होनी चाहिए। उपर्युक्त मौलिक अधिकारों की आलोचना तथा उसके उत्तर से स्पष्ट है कि जो प्रतिबन्ध इन अधिकारों पर लगाए गए हैं, वे उचित हैं।
प्रश्न 6.
सम्पत्ति के अधिकार पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अथवा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य किन शर्तों पर व्यक्तिगत सम्पत्ति को ग्रहण कर सकता है?
उत्तर:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार (Authority of Law) के बिना उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद के अनुसार ही सार्वजनिक हित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं किया जा सकता और ऐसे कानून द्वारा उस सम्पत्ति के प्रति मुआवज़ा देने की व्यवस्था होनी चाहिए अथवा उन सिद्धान्तों का वर्णन होना चाहिए, जिनके आधार पर मुआवजा दिया जाता हो।
प्रथम संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 31-A तथा 31-B को अनुच्छेद 31 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 31-A द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि किसी राज्य का कोई कानून (पिछला या भविष्य में) किसी भी सम्पत्ति या जमींदारी प्रथा के मौलिक अथवा मध्यस्थ अधिकार पर प्रभाव डाले या कुछ समय के लिए किसी के अधिकारों को नियन्त्रित करे या उन अधिकारों को समाप्त करे या सार्वजनिक हित में उस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध करने के लिए, कुछ काल के लिए किसी की सम्पत्ति पर कब्जा करे तो ऐसी किसी भी अवस्था में न्यायालय उस राज्य के अधिकार को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं करेंगे कि यह अधिकार या कब्जा संविधान के उन अधिकारों के विरुद्ध है जो अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 में प्रदान किए गए हैं।
अनुच्छेद 31-B ने संविधान के साथ 9वीं अनुसूची जोड़ी जिसमें जमींदारी प्रथा समाप्त करने सम्बन्धी 13 जमींदारी उन्मूलन कानून दर्ज किए, जिन्हें 31-A उपबन्ध के अभाव में अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती थी। इस सूची के लिए व्यवस्था हुई कि ये कानून इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किए जाएँगे कि इनका कोई उपबन्ध संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में से किसी के उलट है। अनुच्छेद 31 (B) द्वारा विधानमण्डल (Competent Legislature) की 9वीं सूची में दर्ज किसी भी अधिनियम को समाप्त अथवा संशोधित करने की शक्ति भी मिली।
25वें संशोधन द्वारा ‘मुआवज़ा’ (Compensation) शब्द के स्थान पर ‘रांशि’ (Amount) शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि सार्वजनिक हित के लिए प्राप्त सम्पत्ति के बदले दी जाने वाली राशि को इस न्यायालय में चुनौती न दी जा सके कि राशि अपर्याप्त है। 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31-C को जोड़ा गया।
44वें संशेधन द्वारा अनुच्छेद 31 को संविधान में से निकाल दिया गया है परन्तु 31-A, 31-B, 31-C को वही रहने दिया गया है। अतः इस संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में से निकाल दिया गया है और सम्पत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार बन गया है। परन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालने का प्रभाव अल्पसंख्यकों की संस्थाओं की स्थापना तथा उनके संचालन के अधिकार पर नहीं पड़ना चाहिए। 44वें संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद 300-A शामिल किया गया है जो यह घोषणा करता है कि कानून के आदेश के बिना किसी को भी उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 7.
भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का महत्त्व बताइए।
अथवा
नागरिकों की उन्नति और विकास के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
मौलिक अधिकारों का महत्त्व (Importance of Fundamental Rights)-व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए मौलिक अधिकारों का बहुत महत्त्व है। यदि व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान न किए जाएँ, तो उसके जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की रक्षा का कोई उपाय न रहे। मौलिक अधिकार सरकार तथा विधानमण्डल को तानाशाह बनने से रोकते हैं. और व्यक्ति को आत्म-विकास का अवसर प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में विशेष महत्त्व है। मौलिक अधिकार वास्तव में लोकतन्त्र की आधारशिला हैं। मौलिक अधिकारों के महत्त्व का वर्णन निम्नलिखित है
1. मौलिक अधिकारों द्वारा सामाजिक समानता की स्थापना होती है (Social Equality is Established by the Fundamental Rights):
मौलिक अधिकारों द्वारा सामाजिक समानता की स्थापना होती है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए गए हैं। धर्म, जाति, भाषा, रंग-लिंग आदि के आधार पर सबको सामाजिक समानता प्राप्त हो तथा जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हो।
मौलिक अधिकार विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं तथा जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। समानता, स्वतन्त्रता तथा भ्रातृत्व लोकतन्त्र की नींव हैं। भारतीय संविधान द्वारा ये तीनों प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अतः इस तरह से भारत में मौलिक अधिकार यहाँ के लोकतन्त्र की आधारशिला हैं।
2. मौलिक अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं (Fundamental Rights Establish Rule of Law):
भारत में मौलिक अधिकार कानून के शासन की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकारों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।
जो व्यक्ति कानून को तोड़ता है, उसे कानून के अनुसार दण्ड दिया जाता है। कानून जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई मतभेद नहीं करता। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन और निजी स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। शासन कानून के अनुसार चलाया जाता है, न कि किसी व्यक्ति की इच्छानुसार।
3. मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं (Fundamental Rights check the Despotism of the Government):
मौलिक अधिकारों का महत्त्व इस बात में भी निहित है कि ये अधिकार एक ओर तो कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका को उनके निश्चित अधिकार क्षेत्रों में रहने का निर्देश देते हैं और इस प्रकार अधिकारों को उनके अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षित रखते हैं।
दूसरी ओर ये अधिकार नागरिकों को सरकार के निरंकुश शासन के विरुद्ध जनमत को संगठित करने का अवसर प्रदान करते हैं। श्री ए०एन० पालकीवाला के अनुसार, “मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश स्वरूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाले कवच होते हैं।” हमारे देश में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारें शासन चलाने के लिए अपनी इच्छानुसार कानून नहीं बना सकतीं, बल्कि उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
4. मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों तथा सामाजिक हितों में उचित सामञ्जस्य स्थापित करते हैं (Co-ordinate Individual and Social Interests) मौलिक अधिकारों द्वारा व्यक्तिगत हितों तथा सामाजिक हितों में उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए काफी सीमा तक सफल प्रयास किया गया है।
5. मौलिक अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं (Fundamental Rights Establish Rule of Law):
मौलिक अधिकारों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये कानून के शासन की स्थापना करते हैं, जिससे सबको समान न्याय प्राप्त होता है।
6. मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं (Fundamental Rights Protect the interests of Minorities):
अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन करने का अधिकार भी उनको प्राप्त है।
सरकार अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। निष्कर्ष (Conclusion) यह कहना कि मौलिक अधिकारों का कोई महत्त्व नहीं है, एक बड़ी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सन् 1950 में लीनर नामक पत्रिका ने मौलिक अधिकारों के विषय में कहा था, “व्यक्तिगत अधिकारों पर लेख जनता को कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता की सम्भावना के विरुद्ध आश्वासन देता है। इन मौलिक अधिकारों जिसकी कोई भी बुद्धिमान राजनीतिज्ञ उपेक्षा नहीं कर सकता।” मौलिक अधिकारों का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में विशेष महत्त्व है। मौलिक अधिकार वास्तव में लोकतन्त्र की आधारशिला हैं।

प्रश्न 8.
भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अथवा
मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं? इनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आप किन अनुच्छेदों पर इनकी आलोचना कर सकते हैं?
उत्तर:
मौलिक रूप में भारतीय संविधान में अधिकारों सम्बन्धी अनुच्छेद 14 से 32 तक सात प्रकार के मौलिक अधिकार अंकित किए गए थे, परन्तु इन अधिकारों के साथ भारतीय नागरिकों के किसी भी प्रकार के कर्तव्य निश्चित नहीं किए गए थे। काँग्रेस दल के प्रधान श्री डी०के० बरुआ द्वारा सवैधानिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए फरवरी, 1976 में एक 9 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व रक्षा मन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह थे।
काफी तर्को के बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1976 में पेश की। अपनी रिपोर्ट में स्वर्ण समिति ने यह सिफारिश की कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एक अध्याय शामिल किया जाए। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4-A मौलिक कर्तव्य (Part IV-A, Fundamental Duties) अंकित किया गया है। इस नए भाग में भारतीय नागरिकों के दस प्रकार के मौलिक कर्त्तव्य अंकित किए गए हैं। इन दस प्रकार के कर्तव्यों का वर्णन निम्नलिखित है
1. संविधान का पालन तथा राष्ट्र-थ्वज व राष्ट्र-गान का आदर करना (To abide by the Constitution and Respect its Ideals and Institutions like National Flag and National Anthem):
भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान में निहित आदर्शों का पालन करे और देश की सर्वोच्च संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज तथा राष्ट्र-गान का आदर करे। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन करना सरकार का ही नहीं, नागरिकों का भी कर्तव्य है। इसी प्रकार राष्ट्र-गान तथा राष्ट्र-ध्वज का आदर करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
2. भारतीय प्रभुसत्ता, एकता व अखण्डता का समर्थन तथा रक्षा करना (To Uphold and protect the Sovereignty unity and Integrity of India): प्रत्येक नागरिक के लिए यह कर्त्तव्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इस पर नहीं चलेंगे तो कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद प्राप्त हुई स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता खतरे में पड़ सकती है। राष्ट्रीय एकता, देश की अखण्डता और राज्य की प्रभुसत्ता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
3. देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में भाग लेना (To defend the Country and render National Service when called upon to do so):
जिस देश के नागरिक देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहेंगे, वह देश कभी गुलाम नहीं बन सकता। सबका कर्त्तव्य है कि देश की रक्षा करें और समय आने पर अनिवार्य सेवा के लिए सबको तैयार रहना चाहिए।
4. भारत में सब नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना विकसित करना (To promote Spirit of Brotherhood amongest all citizens):
राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यह लिखा गया है, “प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषायी तथा क्षेत्रीय या वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत के सब लोगों में समानता तथा भ्रातृत्व की भावना विकसित करे।” नारियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में अंकित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह उन प्रथाओं का त्याग करे जिनसे नारियों का अनादर होता है।
5. स्वतन्त्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को मानना तथा उनका प्रसार करना (To accept and follow the Noble Ideals which Inspired our National Struggle for the freedom):
प्रत्येक नागरिक का परम कर्त्तव्य है कि जिन आदर्शों, जैसे स्वतन्त्रता, धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र, अहिंसा, राष्ट्रीय एकता, विश्व-बन्धुत्व आदि, के लिए स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया और जिनके लिए शहीदों ने अपना बलिदान किया, उन्हें अपनाएँ और उन पर चलते हुए राष्ट्र का विकास करें।
6. लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना (To Develop Scientific Attitude in the People):
आधुनिक युग विज्ञान का युग है, परन्तु भारत की अधिकांश जनता आज भी अन्धविश्वासों के चक्कर में फंसी हुई है। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है जिस कारण वे अपने व्यक्तित्त्व तथा अपने जीवन का ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाते। इसलिए अब व्यवस्था की है, “प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा जाँच करने और सुधार करने की भावना विकसित करे।”
7. प्राचीन संस्कृति की देन को सुरक्षित रखना (To Preserve the Rich Heritage of Composite Culture):
आज आवश्यकता इस बात की है कि युवकों को भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में बताया जाए ताकि युवक अपनी संस्कृति पर गर्व अनुभव कर सकें। इसलिए मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में यह अंकित किया गया है, “प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण संस्कृति तथा शानदार विरासत का सम्मान करे और उसको स्थिर रखे।”
8. व्यक्तिगत तथा सामूहिक यत्नों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के यत्न करना (To Strive towards excellence in spheres of Individual and Collective Activities):
कोई भी समाज तथा देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक कि उसके नागरिकों में प्रत्येक कार्य को करने की लगन तथा श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा न हो। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करने का यत्न करे, ताकि उसका उच्च स्तरों के प्रति ज्ञान निरन्तर बढ़ता रहे और राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो।
9. वनों, झीलों, नदियों तथा जंगली जानवरों की रक्षा करना तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना (To protect and improve the National Environment including Forests, Lakes, Rivers and Wildlife and to have compossion for living creatures):
प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य-जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और सुधार करें तथा जीव-जन्तुओं के प्रति दया की भावना रखें।
10. हिंसा को रोकना तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करना (To safeguard Public Property and Adjure Vio lence) सार्वजनिक सम्पत्ति देश के धन, शक्ति और सम्पन्नता का स्रोत होती है। इसको हानि पहुँचाना एक प्रकार से अपनी सम्पत्ति को हानि पहुँचाना है। हिंसा से नैतिक और मानवीय मूल्यों का पतन होता है तथा देश की प्रगति में बाधा पड़ती है। इसलिए सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा का त्याग करें।
संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अंकित किया जाना एक प्रगतिशील कदम है। संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों की व्याख्या न होना संविधान की महत्त्वपूर्ण कमी थी, जिसे 42वें संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को शामिल करके दूर किया। कोई देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक अपने अधिकार की अपेक्षा अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागृत न हों।
महात्मा गाँधी अधिकारों की अपेक्षा कर्त्तव्यों पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था कि अधिकार कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होते हैं। मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व (Utility and Importance of the Fundamental Duties) मौलिक कर्त्तव्यों की उपयोगिता एवं महत्त्व निम्नलिखित है
1. मौलिक कर्त्तव्य व्यक्ति के आदर्श व पथ-प्रदर्शक हैं (The Fundamental Duties are the Ideals and Guidelines for the Individual)-भारत के संविधान में सम्मिलित किए गए मौलिक कर्त्तव्य आदर्शात्मक हैं। इन कर्त्तव्यों का उद्देश्य कोई स्वार्थ न होकर नागरिकों के दिलों में देश-हित की भावना जागृत करना है। इसके साथ ही ये कर्तव्य नागरिकों का पथ-प्रदर्शन करते हैं।
आज समाज के चारों तरफ स्वार्थ और भ्रष्टाचार का वातावरण फैला हुआ है तथा व्यक्ति व समाज के हितों में उचित सामंजस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जहाँ व्यक्ति स्वहित को प्राथमिक और समाज के हितों को गौण मानता है तो ऐसे समाज के लिए ये मौलिक कर्तव्य जनता का मार्गदर्शन करते हैं और उनके व्यवहार के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं, ताकि वे निजी स्वार्थ की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर सामूहिक हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें।
2. मौलिक कर्त्तव्य नागरिकों में चेतना उत्पन्न करेंगे (The Fundamental Duties will Create Consciousness Among the People):
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने से नागरिकों में अपने कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत होगी और लोगों का श्रेष्ठ आचरण सम्भव हो सकेगा। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत उन्नति तथा विकास के साथ-साथ समाज और देश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करते समय हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि अगर लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख लेंगे तो हम तुरन्त एक शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण क्रान्ति देख सकेंगे। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों के अंकित किए जाने से ये नागरिकों को सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उनके अधिकारों के साथ-साथ कुछ कर्त्तव्य भी हैं।
3. मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में सहायक (Helpful in Attaining the Fundamental Rights):
कर्त्तव्यों की तीसरी महत्ता है कि ये भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि कई ऐसे अधिकार हैं जो कर्त्तव्यों को निभाने मात्र से ही प्राप्त हो जाएँगे।
4. मौलिक कर्त्तव्य का नैतिक महत्त्व (Moral Importance of Fundamental Duties):
यद्यपि यह ठीक है कि इन कर्तव्यों के पीछे किसी प्रकार की कानूनी शक्ति नहीं है, फिर भी इनकी नैतिक महत्ता है। कर्तव्यों का नैतिक स्वरूप अपना विशेष महत्त्व रखता है।
5. कमी को पूरा करते हैं (Remove Deficiency):
भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीय नागरिक केवल अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक थे तथा अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। अतः इन मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन द्वारा शामिल करके इस कमी को पूरा कर दिया गया है। मौलिक कर्त्तव्य प्रारम्भिक कमी को पूरा करते हैं।
6. कर्त्तव्य विवाद रहित हैं (Duties are Non-controversial):
भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए मौलिक कर्त्तव्य विवाद रहित हैं। इस पर विभिन्न विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। सभी विद्वानों ने इन कर्त्तव्यों को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बताया है। सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इन कर्तव्यों का पालन भारतीय विकास में सहायक होगा। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना (Criticism of the Fundamental Duties) मौलिक कर्तव्यों की आलोचना इस प्रकार हैं
1. कुछ मौलिक कर्त्तव्य अस्पष्ट हैं (Some of the Fundamental Duties are not Clearly Defined):
आलोचकों का कहना है कि संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिनका अर्थ एकदम स्पष्ट हो। परन्तु ‘कर्तव्यों’ वाले भाग में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका मनमाना अर्थ लगाया जा सकता है, जैसे मिली-जुली संस्कृति (Composite Culture), वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), अन्वेषण और सुधार की भावना (Spirit of Enquiry and Reform) तथा मानववाद आदि।
कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई दण्डात्मक व्यवस्था नहीं है (There is no Coercive Machinery for the Enforcement of the Duties): स्वर्णसिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दण्ड दिया जाए और उसके लिए संसद उचित कानूनों का निर्माण करे, परन्तु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वास्तव में कर्तव्यों के वर्तमान रूप को देखते हुए दण्ड की व्यवस्था की ही नहीं जा सकती। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, कर्तव्यों के स्वरूप नितान्त अस्पष्ट हैं, अतः नागरिकों को किस आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।।
3. केवल उच्च आदर्श (High Ideals Only):
मौलिक कर्तव्यों की आलोचना तीसरे स्थान पर की जा सकती है कि ये केवल मात्र उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भारत की अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जो इन उच्च आदर्शों को समझने में असमर्थ है।
4. संविधान के तीसरे अध्याय में सम्मिलित होने चाहिएँ (Should have been Included in Chapter No. Three):
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अध्याय चार में शामिल किया गया है, जबकि इन्हें मौलिक अधिकारों वाले अध्याय तीन में ही रखा जाना चाहिए क्योंकि अधिकारों के साथ ही कर्तव्य अच्छे लगते हैं।
5. महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्यों का छोड़ा जाना (Some Important Duties have been Left):
मौलिक कर्तव्यों की आलोचना आलोचकों के द्वारा इस आधार पर की गई है कि कई महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्यों को कर्तव्यों की सूची में लिखा नहीं गया है, जैसे अनिवार्य मतदान, अनिवार्य सैनिक सेवा, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना आदि को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए था। इन कर्तव्यों को सूची से बाहर रखा जाना विचित्र-सा लगता है।
प्रश्न 9.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों से क्या अभिप्राय है? निदेशक सिद्धान्तों के स्वरूप का विवेचन कीजिए। अथवा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का अर्थ लिखकर उनके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अथवा राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्तों की प्रकृति का वर्णन करें।
उत्तर:
हमारे संविधान-निर्माताओं ने इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा और संविधान के चौथे अध्याय (Chapter IV) में कुछ ऐसे सिद्धान्तों का वर्णन किया जो राज्य के पथ-प्रदर्शन का कार्य करते रहें। इन सिद्धान्तों के पीछे कानून की शक्ति नहीं है अर्थात् इन सिद्धान्तों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, परन्तु यह बात हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है कि राज्य की नीति के इन निदेशक सिद्धान्तों का शासन-व्यवस्था में मौलिक रूप से पालन किया जाएगा। भले ही ये सिद्धान्त कानूनी रूप में लागू न किए जा सकते हों, परन्तु इन्हें व्यवहार में लागू करने के लिए जनमत (Public Opinion) का हाथ अधिक मात्रा में होगा।
हमारे संविधान में इन सिद्धान्तों को राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों (Directive Principles of State Policy) का नाम दिया गया है। इनके नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सिद्धान्त राज्य का पथ-प्रदर्शन करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का कथन था कि देश में राजनीतिक प्रजातन्त्र के साथ आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातन्त्र का होना भी आवश्यक है, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकता है।
राज्य-नीति निदेशक सिद्धान्त उन साधनों तथा नीतियों को बताते हैं, जिनका पालन करके भविष्य में भारत में एक क-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना की जा सके। एम०बी० पायली के शब्दों में, “सामूहिक रूप से सिद्धान्त लोकतन्त्रात्मक भारत का शिलान्यास करते हैं। ये भारतीय जनता के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का वह भाग है जिन्हें वह एक सीमित अवधि के भीतर प्राप्त करना चाहती है।”
दूसरे शब्दों में, राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त वे आदेश-पत्र हैं, जिनको राज्य की व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका को कोई भी कानून या नीति बनाते समय ध्यान में रखना पड़ता है। डॉ० अम्बेडकर (Dr. Ambedkar) ने संविधान सभा में कहा था, “संविधान के इस भाग को अधिनियमित कर भविष्य में सभी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका को यह निर्देश दिया गया है कि वे किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।”
निदेशक सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
1. आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित (Inspired from Irish Constitution):
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित कहे जा सकते हैं। आयरलैण्ड के संविधान में भी राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त पाए जाते हैं, परन्तु भारतीय व्यवस्था आयरिश व्यवस्था से कुछ भिन्न; जैसे भारत और आयरलैण्ड में निदेशक तत्त्वों की प्रकृति समान नहीं है तथा भारत में निदेशक तत्त्व राज्य के लिए निर्देश हैं, जबकि आयरलैंड में केवल विधायकों के लिए निर्देश हैं।
2. शासन-व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त (Fundamental Principles for Governance of the State):
राज्य के निदेशक तत्त्व शासन-व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्त हैं। संविधान की अनुच्छेद 37 में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि ये सिद्धान्तवाद योग्य नहीं हैं तो भी राज्य के प्रशासन हेतु आधारभूत हैं, जिनके आधार पर राज्य को कानून बनाने चाहिएँ।।
3. समाजवादी व्यवस्था के आधार (Basis of Socialist System):
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त समता पर आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करते हैं जिसमें आर्थिक विषमता व असमानता को दूर करने की बात कही गई है। इसलिए आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings) ने नीति-निदेशक सिद्धान्तों के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, “संविधान के ये पन्ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किए बिना ही लोकतान्त्रिक समाजवाद की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं।”
4. भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप (In accordance with Indian Social Background):
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हैं, जैसे इनमें बहुधर्मी समाज होने के नाते समान नागरिक आचार संहिता. गरीबी के दृष्टिकोण से मुफ्त कानूनी सहायता, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के विकास के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध इत्यादि को लागू करने के लिए कहा गया है।
5. व्यापक क्षेत्र (Wide Scope):
निदेशक सिद्धान्तों का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक न्याय से सम्बन्धित तत्त्वों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय, गाँधीवादी पंचायत व्यवस्था, मद्य-निषेध, जंगली जीवों व पर्यावरण की रक्षा सम्बन्धी तत्त्व भी पाए जाते हैं। इस प्रकार निदेशक सिद्धान्त समाज के सभी पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरण तथा इतिहास से सम्बन्धित हैं।
6. सकारात्मक प्रकृति (Positive Nature):
निदेशक सिद्धान्त की प्रकृति सकारात्मक है जो राज्य को निदेशक तत्त्वों के अनुसार कार्य करने का निर्देश देती है, जैसे राज्य गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे, राज्य ऐसी नीतियाँ बनाए, जिनसे सभी नागरिकों को, स्त्री व पुरुषों को समान रूप से जीवनयापन के उचित साधन उपलब्ध हो सकें, इत्यादि।
7. मौलिक अधिकारों के पूरक (Complementary of Fundamental Rights):
नागरिकों को मौलिक अधिकार यथार्थ में तभी प्राप्त हो सकते हैं, जबकि नीति-निदेशक तत्त्वों को लागू किया जाए। राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत ही मौलिक अधिकारों की प्राप्ति सम्भव है। इसलिए न्यायपालिका ने बार-बार अनेक निर्णयों में कहा है कि नीति-निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।
8. आदर्शवादी (Idealistic):
नीति-निदेशक सिद्धान्त यथार्थवादी ही नहीं हैं, बल्कि उनमें आदर्श भी निहित हैं, जैसे विश्व-शान्ति का आदर्श, वन्य जीवों की रक्षा का आदर्श इत्यादि।
9. लोक-कल्याणकारी राज्य के आधार (Basis of Welfare State):
अनुच्छेद 38 में प्रतिपादित नीति-निदेशक सिद्धान्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 39 का सम्बन्ध उन नीतियों से है जो लोक-कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।
10. न्याय-योग्य नहीं (Non-Justiceable):
अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये निदेशक सिद्धान्त वाद-योग्य नहीं हैं अर्थात् नागरिक इन तत्त्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय सरकार को इन सिद्धान्त को लागू करने लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता, लेकिन वाद-योग्य न होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि नागरिक इन सिद्धान्त के आधार पर किसी कानून तथा शासकीय कार्य को चुनौती नहीं दे सकते और न्यायालय इन सिद्धान्त के आधार पर निर्णय नहीं दे सकते।
नागरिक इन सिद्धान्त के आधार पर कानूनों तथा प्रशासकीय कार्यों को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और न्यायालय इन सिद्धान्त के आधार पर निर्णय दे सकते हैं, केवल इन सिद्धान्त को लागू करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते।
11. ये सिद्धान्त किसी विशेष राजनीतिक विचारअनुच्छेद से सम्बन्धित नहीं हैं (These Principles are not connected with any particular theory):
नीति-निदेशक सिद्धान्तों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये किसी विशेष विचारअनुच्छेद से बँधे हुए नहीं हैं। ये सिद्धान्त बहुत लचीले हैं और किसी भी विचारअनुच्छेद के माध्यम से इनकी पूर्ति हो सकती है। वास्तव में राजनीतिक लोकतन्त्र के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास के कारण इन्हें विचारअनुच्छेदों के बन्धन से मुक्त रखा गया है।
प्रश्न 10.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त क्या हैं? हमारे संविधान में दिए गए राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए। इन्हें कैसे मनवाया जा सकता है?
अथवा
भारतीय संविधान में दिए गए किन्हीं पाँच राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
संविधान के अध्याय IV में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। अध्ययन के लिए इन्हें प्रायः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है-
- समाजवादी सिद्धान्त (Socialist Principles),
- गाँधीवादी सिद्धान्त (Gandhian Principles),
- उदारवादी लोकतन्त्रीय सिद्धान्त (Liberal Democratic Principles)। इन तीन वर्गों में एक और वर्ग भी जोड़ा जा सकता है-
- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी सिद्धान्त (Principles Relating to International Relations) स्मरण रहे कि संविधान में इनका वर्णन इन विभिन्न रूपों में विभाजित करके नहीं किया गया है
1. समाजवादी सिद्धान्त (Socialist Principles)- इस वर्ग के अधीन ऐसे सिद्धान्त रखे जा सकते हैं जिनका उद्देश्य भारत में समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ऐसे सिद्धान्त हैं-
(1) राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा जिससे
(क) सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीविका उपार्जन के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें,
(ख) समान काम के लिए सभी को समान वेतन मिले,
(ग) देश के भौतिक तथा उत्पादन के साधनों का विभाजन इस प्रकार हो कि सार्वजनिक हित का पालन हो,
(घ) धन का उचित वितरण हो तथा केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में धन का केन्द्रीयकरण न हो,
(ङ) मजदूरों, स्त्रियों तथा बालकों की परिस्थितियों का दुरुपयोग न हो और वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर कोई ऐसा कार्य न करें जो उनकी शक्ति से बाहर हो तथा जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो,
(2) मजदूरों को काम करने की न्यायपूर्ण तथा मानवीय परिस्थितियाँ प्राप्त हों तथा स्त्रियों को प्रसति सहायता मिले। राज्य हर प्रकार से यह प्रयत्न करे कि राज्य से बेकारी और बीमारी दूर हो। बूढ़ों और दिव्यांगों को सार्वजनिक सहायता दी जाए,
(3) राज्य में अधिक-से-अधिक नागरिकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए,
(4) राज्य यह प्रयत्न करेगा कि सभी कर्मचारियों, जो किसी भी उद्योग, कृषि अथवा धन्धे में लगे हों, को काम का उचित वेतन तथा काम की उचित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हों, जिनसे वे अपना जीवन-स्तर ऊँचा कर सकें।
2. गाँधीवादी सिद्धान्त (Gandhian Principles)-संविधान-निर्माताओं ने गाँधी जी के विचारों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किए हैं-
(1) राज्य गाँवों में पंचायतों को संगठित करे तथा उनको इतनी शक्तियाँ दे जिनसे कि वे प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें,
(2) राज्य समाज के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा कबीलों की शिक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषप
(3) गाँवों में घरेलू दस्तकारियों की उन्नति के लिए प्रयत्न करेगा,
(4) राज्य नशीली वस्तुओं के सेवन को रोकने का प्रयत्न करेगा,
(5) राज्य कृषि तथा पशुपालन उद्योग का संगठन वैज्ञानिक अनुच्छेदों पर करने का प्रयत्न करेगा। दूध देने वाले पशुओं को मारने पर रोक लगाएगा और पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न करेगा।
3. उदारवादी लोकतन्त्रीय सिद्धान्त (Liberal Democratic Principles)
- राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उचित कदम उठाएगा,
- संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर-अन्दर राज्य 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करेगा,
- राज्य समस्त भारत में सामान्य व्यवहार नियम (Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयत्न करेगा,
- राज्य लोगों के जीवन-स्तर तथा आहार-स्तर को ऊँचा उठाने तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार करने का यत्न करेगा,
- राज्य ऐतिहासिक अथवा कलात्मक दृष्टि से महत्त्व रखने वाले स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की रक्षा करेगा और उनको नष्ट होने अथवा कुरूप होने से बचाएगा।
4. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्बन्धित सिद्धान्त (Principles Relating to International Relations)- नीति-निदेशक सिद्धान्त राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नीति से भी सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य-
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा,
- राष्ट्रों के मध्य उचित व सम्मानपूर्वक सम्बन्ध बनाए रखेगा,
- अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व कानून को सम्मान देगा,
- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने का प्रयास करेगा।
42वें संशोधन द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में वृद्धि (Accretion in Directive Principles of State Policy through 42nd Amendment)42वें संशोधन द्वारा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में निम्नलिखित नए सिद्धान्त शामिल किए गए हैं
(1) राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार से करेगा जिससे कि बच्चों को स्वस्थ, स्वतन्त्र और प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण में अपने विकास के लिए अवसर और सुविधाएँ प्राप्त हों,
(2) राज्य ऐसी कानून प्रणाली के प्रचलन की व्यवस्था करेगा जो समान अवसरों के आधार पर न्याय का विकास करे। राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा,
(3) राज्य कानून द्वारा या अन्य ढंग से श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार बनाने के लिए पग उठाएगा,
(4) राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करने तथा देश के वन और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा।
44वें संशोधन द्वारा राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का विस्तार किया गया है। 44वें संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत एक और निदेशक सिद्धान्त जोड़ा गया है। 44वें संशोधन के अनुसार राज्य, विशेषकर आय की असमानता को न्यूनतम करने और न केवल व्यक्तियों में, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों अथवा व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों में स्तर, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा।
इस तरह राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त जीवन के पहलू के साथ सम्बन्धित हैं, क्योंकि ये सिद्धान्त कई विषयों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए स्वाभाविक ही है कि इनको परस्पर किसी विशेष तर्कशास्त्र के साथ नहीं जोड़ा गया है। यह तो एक तरफ का प्रयत्न था कि इन सिद्धान्तों द्वारा सरकार को निर्देश दिए जाएँ, ताकि सरकार उन कठिनाइयों को दूर कर सके जो उस समय समाज में विद्यमान थीं।
प्रश्न 11.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की आलोचना किस आधार पर की जाती है?
उत्तर:
भारतीय संविधान के अध्याय IV में दिए गए निदेशक सिद्धान्तों की आलोचकों द्वारा कटु आलोचना की गई है। इन्हें व्यर्थ व अनावश्यक कहा गया है। संविधान में केवल उन्हीं बातों का वर्णन होता है जिनको व्यवहार में लाया जा सके, परन्तु निदेशक सिद्धान्त ऐसे तत्त्व हैं जिनको तुरन्त व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। सरकार को इन पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
ये कोरे वायदे हैं जो जनता को धोखा देने के लिए संविधान में रखे गए हैं तथा इनकी वास्तविक उपयोगिता कुछ नहीं है। इनका महत्त्व राजनीतिक घोषणाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रो० व्हीयर (Prof. Wheare) ने इन्हें केवल उद्देश्यों व आकांक्षाओं का घोषणा-पत्र कहा है।
श्री के०टी० शाह (K.T. Shah) के अनुसार, “निदेशक सिद्धान्त उस चैक के समान हैं जिसका बैंक ने अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान करना है।” (Directive Principles are like a cheque payable by the bank at its convenience.)
श्री नसीरुद्दीन (Sh. Nasiruddin) ने इनकी तुलना “नए वर्ष के उन प्रस्तावों से की है जो जनवरी के दूसरे दिन ही तोड़े जा सकते हैं।” (New years resolutions which can be broken on the second of January.) आलोचना निम्नलिखित अनुच्छेदों पर की गई है
1. इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है (They are not backed by Legal Sanctions):
निदेशक सिद्धान्तों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है तथा सरकार को इन पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये न्यायसंगत नहीं हैं। इनको व्यावहारिक रूप देना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।
2. ये अप्राकृतिक हैं (They are Unnatural):
संविधान में इन सिद्धान्तों का सम्मिलित किया जाना अप्राकृतिक प्रतीत होता है। कोई भी प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य अपने आपको इस प्रकार के निर्देश नहीं दे सकता। निर्देश सदा सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधीनस्थ सत्ता को दिए जाते हैं, न कि अपने आपको।
3. ये व्यर्थ हैं (They are Superfluous):
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। इनका पृथक् वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इससे संविधान की जटिलता बढ़ती है।
4. ये स्थाई नहीं हैं (They are not Permanent):
इस प्रकार के सिद्धान्त स्थाई नहीं हो सकते। देश की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं तथा समय और स्थिति की आवश्यकता के अनुसार सिद्धान्तों को बदलना पड़ता है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जो सिद्धान्त 20वीं शताब्दी में उपयोगी समझे गए हैं, वे 21वीं शताब्दी में भी उपयोगी सिद्ध होंगे।
5. कुछ सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं हैं (Some Principles are not Practicable):
निदेशक तत्त्वों में कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनको व्यावहारिक रूप देना कठिन है। उदाहरणतया नशाबन्दी के सिद्धान्त को लागू करने से कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। एक ओर सरकार का राजस्व बहुत कम हो जाता है और दूसरी ओर अवैध शराब का निकालना बढ़ जाता है तथा कई कानूनी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। आलोचकों का कहना है कि राज्य द्वारा लागू की गई नैतिकता कोई नैतिकता नहीं होती।
6. ये प्रकृति में विदेशी हैं (They are Foreigner in Nature):
इन सिद्धान्तों पर विदेशी विचारअनुच्छेद का प्रभाव है। सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) के अनुसार, “इन पर इंग्लैण्ड के 19वीं शताबी के फेबियन समाजवाद (Fabian Socialism) का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। जिन सिद्धान्तों को 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में ठीक माना जाता था, उन्हें 20वीं शताब्दी के भारतीय संविधान में स्थान देना प्रगतिशील व्यवस्था नहीं थी। ये सिद्धान्त भारतीय संस्कृति व परम्परा के अनुकूल नहीं हैं।”
इनका सही ढंग से वर्गीकरण नहीं किया गया है (They are not Properly Classified):
डॉ० श्रीनिवासन (Dr. Srinivasan) के अनुसार, “निदेशक सिद्धान्तों का उचित ढंग से वर्गीकरण नहीं किया गया है और न ही उन्हें क्रमबद्ध रखा गया है। इस घोषणा में अपेक्षाकृत कम महत्त्व वाले विषयों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आर्थिक व सामाजिक प्रश्नों के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें आधुनिकता का प्राचीनता के साथ बेमेल मिश्रण किया गया है। इसमें तर्कसंगत और वैज्ञानिक व्यवस्थाओं को भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण समस्याओं के साथ जोड़ा गया है।”
8. वे अस्पष्ट व दोहराए गए हैं (They are Vague and Repetitive):
ये सिद्धान्त अस्पष्ट व अनिश्चित हैं। इन्हें बार-बार दोहराया गया है। ये सिद्धान्त संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। डॉ० श्रीनिवासन के अनुसार, “इन्हें उत्साहपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये अस्पष्ट व दोहराए गए सिद्धान्त हैं।” ।
9. ये कोरे वायदे हैं (They are Unused Promises):
आलोचकों का कहना है कि निदेशक सिद्धान्त जनता को धोखा देने का साधन मात्र हैं। ये कोरे आश्वासन हैं जिनसे जनसाधारण को सन्तुष्ट रखने का प्रयास किया गया है। इनके द्वारा भोली-भाली जनता को झुठलाने की कोशिश की गई है।
10. इनमें राजनीतिक दार्शनिकता अधिक है व व्यावहारिक राजनीति कम (They are more a Political Philoso phy than a Practical Politics) ये सिद्धान्त शुद्ध आदर्शवाद प्रस्तुत करते हैं। इनका व्यावहारिक राजनीति से बहुत कम सम्बन्ध है।
प्रश्न 12.
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की उपयोगिता तथा महत्त्व का वर्णन करें।
उत्तर:
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की उपयोगिता तथा महत्त्व (Utility and Importance of Directive Principles of State Policy)-राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की काफी आलोचना हुई है और बहुत-से लोगों ने इन्हें केवल नव वर्ष की शुभ कामनाएँ मात्र कहा है, क्योंकि इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय का द्वार नहीं खटखटाया जा सकता।
ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं, परन्तु इनकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता। निदेशक सिद्धान्तों में निहित सामाजिक व आर्थिक लोकतन्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना भारत में लोकतन्त्र सफल हो ही नहीं सकता। निदेशक सिद्धान्तों की उपयोगिता निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होती है
1. ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं (These are Supplement of the Fundamental Rights):
मौलिक अधिकार देश में केवल राजनीतिक लोकतन्त्र (Political Democracy) को स्थापित करते हैं, परन्तु राजनीतिक लोकतन्त्र की सफलता के लिए देश में आर्थिक लोकतन्त्र की व्यवस्था करनी आवश्यक है। आर्थिक लोकतन्त्र के बिना राजनीतिक लोकतन्त्र अधूरा रह जाता है। राजनीतिक लोकतन्त्र में लोगों को राजनीतिक स्वतन्त्रताएँ तो प्राप्त होती हैं, परन्तु उन्हें आर्थिक चिन्ताओं से छुटकारा नहीं मिल पाता।
उन्हें वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं, जिनसे उनका जीवन-स्तर ऊपर उठ सके और वे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो सकें। निदेशक सिद्धान्त भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कमी को दूर करते हैं और उन तत्त्वों को अपनाने के लिए कहते हैं जिन पर चलते हुए इस देश में राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ-साथ आर्थिक लोकतन्त्र की भी स्थापना की जा सके।
2. ये सरकारों के लिए निर्देश हैं (They are Directives to Governments):
ये सिद्धान्त केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय सरकारों का मागदर्शन करते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि संविधान में निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या-क्या कार्य करने हैं। इन सिद्धान्तों की तुलना 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नर जनरल व गवर्नरों को जारी किए गए उन निर्देश-पत्रों से की जा सकती है जिनमें उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए जाते थे।
अन्तर केवल इतना है कि इन निर्देश-पत्रों में निर्देश विधानपालिका व कार्यपालिका दोनों को दिए गए हैं, जबकि नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्देश केवल कार्यपालिका को ही दिए जाते हैं। श्री एम०सी० सीतलवाद (M.C. Setalvad) के अनुसार, “वे संघ में समस्त अधिकारी वर्ग को दिए गए निर्देश-पत्र या सामान्य सिफारिशों के समान प्रतीत होते हैं जो उन्हें उन आधारभूत सिद्धान्तों की याद दिलाते हैं जिनके आधार पर संविधान का उद्देश्य नई सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है।”
3. ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं (They are Positive Obligations of State):
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त राज्य की सकारात्मक ज़िम्मेदारियाँ बतलाते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन (Granville Austin) के शब्दों में, “राज्य के सकारात्मक दायित्व निश्चित करते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की भावी सरकारों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी कि वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सार्वजनिक भलाई के बीच तथा कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति व विशेषाधिकार और सभी लोगों को लाभ पहुँचाने के बीच का मार्ग निकालें, ताकि सभी लोगों की शक्तियों को समान रूप से सभी लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जा सके।”
4. ये सामाजिक क्रांति का आधार हैं (These are basis of Social Revolution):
राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त नई सामाजिक दशा के सूचक हैं। वे सामाजिक क्रांति का आधार हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन (Granville Austin) के अनुसार, “निदेशक सिद्धान्तों में सामाजिक क्रांति का स्पष्ट विवरण मिलता है। वे भारतीय जनता को सकारात्मक अर्थ में स्वतन्त्र करते हैं। वे उन्हें समाज और प्रकृति द्वारा उत्पन्न की गई शताब्दियों की निष्क्रियता से मुक्ति दिलाते हैं। वे उन्हें उन घृणित शारीरिक परिस्थितियों से मुक्त कराते हैं जिन्होंने उन्हें अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने से रोके रखा था।”
5. इन सिद्धान्तों के पीछे जनमत की शक्ति है (These Principles are backed by Public Opinion):
ये सिद्धान्त न्याय-संगत नहीं हैं, परन्तु इनके पीछे लोकमत की शक्ति है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कोई भी सरकार लोकमत की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करेगी तो वह लोगों का विश्वास खो बैठेगी और अगले आम चुनाव में उसकी हार अवश्य होगी।
प्रो० पायली के अनुसार, “ये निर्देश राष्ट्र की आत्मा का आधारभूत स्तर हैं तथा जो इनका उल्लंघन करेंगे, वे अपने आप को जिम्मेदार स्थान (Position of Responsibility) से हटाने का खतरा मोल लेंगे जिसके लिए उन्हें चुना गया है।”
6. ये सरकार की नीतियों में स्थिरता बनाए रखते हैं (These maintain stability in the Policies of Govt.):
संसदीय शासन-प्रणाली में सरकारें बदलती रहती हैं, परन्तु जो भी सरकार सत्तारूढ़ होगी, वह इन सिद्धान्तों पर चलने के लिए बाध्य होगी। इस प्रकार सरकार की मूल नीतियों में निरन्तरता व स्थिरता बनी रहेगी।
7. ये सिद्धान्त शैक्षणिक महत्त्व रखते हैं (These Principles have an Educative Value):
ये सिद्धान्त आने वाली पीढ़ियों के नवयुवकों को इस बात की शिक्षा देंगे कि हमारे संविधान-निर्माता देश में किस प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे तथा इस बारे में क्या कछ किया जा चका है और क्या कछ करना बाकी है। प्रो० एम०वी० पायली (Prof. M.V. Pylee) के अनुसार, “वे भविष्य के नवयुवकों के मन व विचारों में स्थिर व गतिशील राजनीतिक व्यवस्था के मूल तत्त्वों को स्थान देंगे।” .
8. कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक (Helpful for Establishment of a Welfare State):
आज कल्याणकारी राज्य का युग है और इन सिद्धान्तों में ही कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा की गई है। इन्हें लागू करके ही भारत को एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति संपू (Justice Sapru) ने कहा है कि राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में वे सभी बातें विद्यमान हैं जिनके आधार पर किसी भी आधुनिक जाति में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की. जा सकती है।
9. आर्थिक लोकतन्त्र हेत (For Economic Democracy):
आर्थिक लोकतन्त्र के अभाव में राजनीतिक लोकतन्त्र अर्थहीन है। आर्थिक लोकतन्त्र को निदेशक तत्त्वों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डॉ० अम्बेडकर के शब्दों में, “प्रत्येक सरकार आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए प्रयास करेगी। इसी उद्देश्य से संविधान के चौथे भाग में कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।”
10. संविधान का पालन (Enforcement of Constitution):
संविधान का पालन निदेशक तत्त्वों के पालन में ही हेत है। डॉ० अल्लादि कृष्णास्वामी का कथन है, “यदि राज्य इन आदर्शों की उपेक्षा करता है तो व्यावहारिक रूप से यह स्वयं संविधान की उपेक्षा करने के समान होगा।”
11. न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक (Guide for Judiciary):
भारतीय न्यायपालिका ही कानूनों तथा संविधानों की व्यवस्था का अधिकार रखती है। बेशक ये सिद्धान्त न्यायालयों के माध्यम से लागू नहीं करवाए जा सकते, परन्तु इन्होंने कानूनों तथा संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका का मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में इनका उल्लेख भी कर दिया है।
12. सरकार की नीति में निरन्तरता तथा स्थिरता (Continuity and Stability in Policies of the Government):
वैसे तो जब भी सत्ता में परिवर्तन होता है और दूसरे दल के हाथ में सत्ता आती है तो वह अपनी नीति निश्चित करता है, परन्तु इन सिद्धान्तों के कारण सरकार की नीति में निरन्तरता काफी मात्रा में बनी रहती है और उसे स्थिरता मिलती है क्योंकि प्रत्येक दल जन-कल्याण की नीति अवश्य अपनाता है और ऐसा करते समय उसे इनका सहारा लेना ही पड़ता है।
13. शासकीय कार्यों के मूल्याँकन हेतु मापदण्ड (Measurement for Evaluation of Government’s Functions):
नीति-निदेशक तत्त्व जनता को शासकीय कार्यों के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड प्रदान करते हैं जिनके आधार पर जनता शासकीय कार्यों का मूल्यांकन कर सकती है। डॉ० अम्बेडकर के शब्दों में, “यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो उसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को निश्चित रूप से जवाब देना होगा।”
निष्कर्ष (Conclusion)-निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में लिखित उद्देश्यों-लोक-कल्याण, लोकतन्त्र, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि को नीति-निदेशक तत्त्वों को लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वाद-योग्य न होने से इनका महत्त्व कम नहीं हो जाता।
वर्तमान में तो न्यायपालिका भी अपने निर्णय इन सिद्धान्तों के आधार पर देने लगी है। इन्हें उसी प्रकार से भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त है, जिस प्रकार इंग्लैण्ड में प्रथाओं को प्राप्त है। भारत का भविष्य इन निदेशक सिद्धान्तों पर ही निर्भर है। एम०सी० छागला (M.C. Chagla) के अनुसार, “यदि इन सिद्धान्तों को ठीक प्रकार से अपनाया जाए तो हमारा देश वास्तव में धरती पर स्वर्ग बन जाएगा।
भारतीयों के लिए लोकतन्त्र तब केवल राजनीतिक अर्थ में ही नहीं होगा, बल्कि यह भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए बना एक ऐसा कल्याणकारी राज्य होगा जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने और अपने श्रम का उचित प्रतिफल पाने का समान अवसर प्राप्त होगा।”
वस्तु निष्ठ प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें
1. मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है-
(A) राष्ट्रपति के द्वारा
(B) संसद के द्वारा
(C) विधानमंडलों के द्वारा
(D) प्रधानमंत्री के द्वारा
उत्तर:
(B) संसद के द्वारा
2. संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था है
(A) अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत
(B) अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत
(C) अनुच्छेद 23 से 25 के अंतर्गत
(D) अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत
उत्तर:
(D) अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत
3. कौन-से संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्य संविधान में अंकित किए गए हैं
(A) 42वें संशोधन द्वारा
(B) 44वें संशोधन द्वारा
(C) 45वें संशोधन द्वारा
(D) 47वें संशोधन द्वारा
उत्तर:
(A) 42वें संशोधन द्वारा

4. संविधान के कौन-से भाग में मौलिक कर्त्तव्य अंकित हैं
(A) भाग तृतीय में
(B) भाग चतुर्थ में
(C) भाग चतुर्थ-ए में
(D) भाग पांचवें में
उत्तर:
(C) भाग चतुर्थ-ए में
5. भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
(A) अनुच्छेद 14 से 31
(B) अनुच्छेद 12 से 35
(C) अनुच्छेद 12 से 35
(D) अनुच्छेद 1 से 32
उत्तर:
(C) अनुच्छेद 12 से 35
6. ‘समानता का अधिकार’ (Right to Equality) में सम्मिलित नहीं है
(A) कानून के समक्ष समानता
(B) अवसर की समानता
(C) सामाजिक समानता
(D) आर्थिक समानता
उत्तर:
(D) आर्थिक समानता
7. कौन-से अनुच्छेद द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की मनाही की गई है?
(A) अनुच्छेद 13 द्वारा
(B) अनुच्छेद 33 द्वारा
(C) अनुच्छेद 35 द्वारा
(D) अनुच्छेद 18 द्वारा
उत्तर:
(A) अनुच्छेद 13 द्वारा
8. निम्नलिखित आदेशों में से कौन-सा आदेश न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी ढंग से नजरबन्द किए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए दिया जाता है?
(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(B) परमादेश
(C) उत्प्रेषण लेख
(D) अधिकार पृच्छा
उत्तर:
(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
9. ‘समानता के अधिकार’ (Right to Equality) की व्यवस्था है
(A) अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत
(B) अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत
(C) अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत
(D) अनुच्छेद 29 से 32 के अंतर्गत
उत्तर:
(A) अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत
10. मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में स्पष्ट वर्णन नहीं है
(A) विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का
(B) धार्मिक स्वतंत्रता का
(C) कानून के समक्ष समानता का
(D) प्रेस की स्वतंत्रता का
उत्तर:
(D) प्रेस की स्वतंत्रता का
11. सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों की भारतीय संविधान में व्यवस्था है
(A) अनुच्छेद 31 व 32 के अंतर्गत.
(B) अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत
(C) अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत
(D) अनुच्छेद 33 व 34 के अंतर्गत
उत्तर:
(C) अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत
12. ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ (Right to Freedom) में सम्मिलित नहीं है
(A) भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता
(B) समुदाय बनाने की स्वतंत्रता
(C) कोई कारोबार करने की स्वतंत्रता
(D) हथियारों सहित एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता
उत्तर:
(D) हथियारों सहित एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता
13. निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्त्तव्य नहीं है?
(A) संविधान का पालन करना
(B) भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन व रक्षा करना
(C) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
(D) माता-पिता की सेवा करना
उत्तर:
(D) माता-पिता की सेवा करना
14. निम्नलिखित में से किस आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को उस कार्रवाई को करने से रोक दिया जाता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से उपयुक्त नहीं है?
(A) परमादेश
(B) प्रतिषेध
(C) उत्प्रेषण
(D) अधिकार पृच्छा
उत्तर:
(D) अधिकार पृच्छा
15. किसके सुझावानुसार निदेशक सिद्धांत संविधान में अंकित किए गए थे?
(A) डॉ० बी०आर० अंबेडकर
(B) डॉ० राजेंद्र प्रसाद
(C) पं० जवाहरलाल नेहरू
(D) सर वी०एन० राव
उत्तर:
(D) सर वी०एन० राव
16. यह किसने कहा था कि “राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांत एक चैक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया है।”
(A) केन्टी० शाह ने
(B) नसीरुद्दीन ने
(C) डॉ० राजेंद्र प्रसाद ने
(D) श्रीमती इंदिरा गांधी ने
उत्तर:
(A) के०टी० शाह ने
17. संविधान में निदेशक सिद्धांत अंकित करने की प्रेरणा मिली थी
(A) 1935 के भारत सरकार कानून से
(B) ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
(C) आयरलैंड के संविधान से
(D) अमेरिका के संविधान से
उत्तर:
(C) आयरलैंड के संविधान से
18. निम्नलिखित में से नीति-निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन-सा है?
(A) पुलिस-राज्य की स्थापना करना
(B) सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना
(C) राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना
(D) समाजवादी राज्य की स्थापना करना
उत्तर:
(B) सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना
19. निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में से कौन-सा उदारवादी है?
(A) काम देने का अधिकार
(B) विश्व-शांति एवं सुरक्षा
(C) समान व्यवहार संहिता
(D) धन केंद्रीकरण पर रोक
उत्तर:
(C) समान व्यवहार संहिता
20. निम्नलिखित निदेशक सिद्धांत सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है
(A) पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान
(B) ग्राम पंचायतों की स्थापना करना कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था
(C) शराब-बंदी लागू करना
(D) कृषि तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करना
उत्तर:
(C) शराब-बंदी लागू करना
21. निम्नलिखित में से किसने नीति-निदेशक सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है?
(A) श्री वी०एन० राय ने
(B) पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
(C) डॉ० बी० आर० अंबेडकर ने
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) डॉ० बी० आर० अंबेडकर ने
22. कौन-से निदेशक सिद्धांतों में भारतीय विदेश नीति के कुछ मूल आधार मिलते हैं?
(A) अनुच्छेद 36 में अंकित निदेशक सिद्धांत में
(B) अनुच्छेद 48 में अंकित निदेशक सिद्धांत में
(C) अनुच्छेद 51 में अंकित निदेशक सिद्धांत में
(D) उपर्युक्त सभी में
उत्तर:
(C) अनुच्छेद 51 में अंकित निदेशक सिद्धांत में
23. “निदेशक सिद्धांतों का कोई महत्त्व नहीं है” यह कथन है
(A) डॉ० बी०आर० अंबेडकर
(B) जैनिंग्स
(C) डॉ० श्रीनिवासन
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(D) इनमें से कोई नहीं ।
24. निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है ?
(A) ग्राम पंचायतों और स्वशासन की समाप्ति
(B) स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन
(C) देश के सभी नागरिकों के लिए आचार संहिता
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(A) ग्राम पंचायतों और स्वशासन की समाप्ति
25. “राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांत नौ वर्षों के प्रस्तावों का संग्रह है।” यह कथन किस विद्वान् का है?
(A) के०सी० ह्वीयर का
(B) नसीरुद्दीन
(C) डॉ० अंबेडकर का
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(B) नसीरुद्दीन
26. निदेशक सिद्धांतों की आलोचना के संबंध में निम्नलिखित ठीक है
(A) अनिश्चित तथा अस्पष्ट
(B) वैधानिक शक्ति का अभाव
(C) पर्याप्त साधनों का अभाव
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
27. निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में एक अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी सिद्धांत है
(A) विश्व-शांति एवं सुरक्षा
(B) ग्राम पंचायतों का संगठन
(C) समान व्यवहार संहिता
(D) समान कार्य, समान वेतन
उत्तर:
(A) विश्व-शांति एवं सुरक्षा
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए-
1. भारतीय संविधान के कौन-से भाग या अध्याय में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है?
उत्तर:
अध्याय तीन में।
2. मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है?
उत्तर:
अनुच्छेद 12 से 35 तक।
3. भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में ‘स्वतंत्रता के अधिकार’ का उल्लेख है?
उत्तर:
अनुच्छेद 19 से 22 तक।
4. भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख कौन-से अनुच्छेद में किया गया है?
उत्तर:
अनुच्छेद 32 में।
5. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई?
उत्तर:
अक्तूबर, 1993 में।
6. कौन-से सवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाला गया?
उत्तर:
44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा।
7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर:
पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एच०एल० दत्तू।
8. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव कौन हैं?
उत्तर:
श्री जयदीप गोविंद।
9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है?
उत्तर:
5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो।
10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं?
उत्तर:
राष्ट्रपति को।
11. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के कौन-से अध्याय में किया गया है?
उत्तर:
अध्याय IV में।
रिक्त स्थान भरें
1. भारतीय संविधान के अध्याय ………… में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
उत्तर:
III
2. भारतीय संविधान का अध्याय …………. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित है।
उत्तर:
IV
3. भारतीय संविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्त ………….. के संविधान से प्रेरित होकर सम्माहित किए गए है।
उत्तर:
आयरलैण्ड
4. वर्तमान में ………….. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।
उत्तर:
श्री एच०एल० दत्तू
5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल ……………. या अधिकतर ……………. तक की आयु तक है।
उत्तर:
5 वर्ष, 70 वर्ष
6. वर्तमान में संविधान में अंकित मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या …………. है।
उत्तर:
11
7. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ………….. में हुआ।
उत्तर:
1993
8. दक्षिण अफ्रीका का संविधान सन् …………. में लागू हुआ।
उत्तर:
1996
9. भारत में शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में …………. संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप दिया गया।
उत्तर:
86वें

10. संविधान के भाग ……………. में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
उत्तर:
IV क (अनुच्छेद 51क)
11. वर्तमान में ……….. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं।
उत्तर:
जयदीप गोविंद
12. …………. ने सवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है।
उत्तर:
डॉ० बी.आर. अम्बेडकर
13. भारतीय संविधान का अनुच्छेद ………….. किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है।
उत्तर:
अनुच्छेद 17
14. भारतीय संविधान का अनुच्छेद ………… सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
उत्तर:
अनुच्छेद 151
![]()
![]()