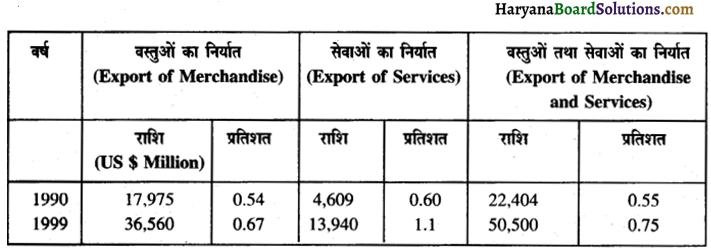Haryana State Board HBSE 12th Class Political Science Important Questions Chapter 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन Important Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Political Science Important Questions Chapter 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन
निबन्धात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन एवं उसमें भारत की स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोक कर विश्व में शान्ति की स्थापना करना है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व राजनीति में बहत महत्त्वपूर्ण परिव मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बदलावों की मांग की जा रही है, क्योंकि बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा इसके अंगों में कुछ दोष उत्पन्न हो गए, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। इसीलिए समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में पुनर्गठन की मांग की जाती रही है।
1. सुरक्षा परिषद् का पुनर्गठन-संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस अंग में सबसे अधिक सुधारों की मांग या पुनर्गठन की बात की जा रही है, वह है, सुरक्षा परिषद् । वास्तव में यह सुरक्षा परिषद् ही है, जहां सदस्य देशों को समान अधिकार नहीं मिले हैं। सरक्षा परिषद में वर्तमान समय में कल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें से 5 स्थाई तथा 10 अस्थाई देश हैं। पांच स्थाई देशों (अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस तथा चीन) को वीटो का अधिकार प्राप्त है जोकि अन्य देशों को प्राप्त नहीं है।
प्राय: यह कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी, जिस अनुपात में महासभा की संख्या बढ़ी है। अतः सुरक्षा परिषद् में और सदस्यों को शामिल किए जाने की माँग की जाती रही है। विश्व के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण देश जैसे भारत, जर्मनी, जापान तथा ब्राज़ील स्थाई सदस्यता के लिए समय-समय पर अपना दावा पेश करते रहें, परन्तु पांचों स्थाई देश ऐसे किसी भी प्रसार का विरोध कर रहे हैं। कुछ सदस्य देशों का तर्क है कि वीटो की धारणा को समाप्त करना चाहिए, परन्तु स्थाई देश इस पर भी सहमत नहीं है। सदस्यता बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा परिषद् में प्रक्रियात्मक, कार्यप्रणाली, पारदर्शिता तथा उत्तरदायी सुधारों की भी आवश्यकता है।
2. महासभा का पुनर्गठन-संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एक अन्य महत्त्वपूर्ण अंग है। यद्यपि महासभा में सभी 193 सदस्य देशों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी इसमें समय-समय पर सुधारों की मांग उठती रही है। रष्ट्र संघ के भतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने यह सझाव दिया है कि महासभा में सर्वसम्मति की प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ देश अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ कोफी अन्नान ने महासभा के प्रस्तावों को लागू करने, महासभा के अध्यक्ष को अधिक शक्तिशाली बनाने पर भी जोर दिया।
3. मानव अधिकार परिषद्-संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग का निर्माण किया था, परन्तु समय-समय पर अमेरिका जैसे देशों ने इस आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया। तत्पश्चात् भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने मानवाधिकार आयोग को समाप्त करके एक छोटे परन्तु दृढ़ मानव अधिकार परिषद् की स्थापना की बात कही। इसके आधार पर एक 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद् बनाई गई।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थाई सेना सम्बन्धी प्रस्ताव-संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोक कर विश्व में शान्ति बनाए रखना है। परन्तु इसकी अपनी स्थायी सेना नहीं है। संकट के समय यह सदस्य देशों की शान्ति सेना का निर्माण करता है, परन्तु इस प्रकार शान्ति सेना के निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है तथा संकट और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कई विद्वान् समय-समय पर यह विचार देते रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी एक स्थाई सेना होनी चाहिए, जो संकट आने पर जल्दी कार्यवाही कर सके।
भारत की स्थिति-ऊपर जितने भी पुनर्गठन एवं सुधारों की चर्चा की गई है, उन सभी में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका एवं स्थिति है, या हो सकती है। भारत सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता का एक मज़बूत उम्मीदवार है और कई देश इसका समर्थन भी कर रहे हैं। महासभा के पुनर्गठन में भारत अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति दर्ज करा सकता है। नई मानवाधिकार परिषद् के 47 सदस्यों में से एक भारत भी है और यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थाई सेना की धारणा वास्तविकता में बदलती है, तो भारत उसमें भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
प्रश्न 2.
विश्व राजनीति में उभरे नए अन्तर्राष्ट्रीय पात्रों की व्याख्या करें।
उत्तर:
विश्व राजनीति में कुछ नए अन्तर्राष्ट्रीय पात्रों का उदय हुआ है, जिन्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों एवं स्वयं सेवी संगठनों (N.G.O.) के रूप में पहचान सकते हैं।
1. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन (International Economic Organisation):
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरे नये अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का वर्णन इस प्रकार है
(1) गैट समझौता (Gatt Agreement):
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् गैट समझौते को सबसे पहला आर्थिक समझौता कहा जा सकता है। गैट समझौते की शुरुआत 1947 में हुई। इसे डंकल समझौता भी कहा जाता है।
(2) विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-W.T.O.):
1 जनवरी, 1995 को गैट समझौते का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 161 है। यह संगठन विश्व स्तर पर व्यापार के नियमों को निश्चित करता है।
(3) यूरोपीयन संघ (European Union):
यूरोपीयन संघ यूरोप का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में की गई। आज युरोपीयन संघ को विश्व में प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है।
(4) आसियान (ASEAN):
आसियान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में की गई। आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाना है।
(5) सार्क (SAARC):
सार्क अर्थात् दक्षिण-एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया के आठ देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। सार्क का उद्देश्य सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
2. गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organisation-N.G.0.):
गैर-सरकारी संगठनों को भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरे नये पात्रों के रूप में पहचाना जाता है। गैर-सरकारी संगठन उन्हें कहा जाता है, जो सरकार के संगठन के भाग नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 71 के अनुसार, “गैर-सरकारी संगठन वह है, जो न सरकार है और न ही सदस्य राज्य, उनकी भूमिका केवल सलाहकारी होती है।”
गैर-सरकारी संगठनों को 20वीं शताब्दी में अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ, जब ऐसा प्रतीत होने लगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियां एवं समझौते तथा विश्व व्यापार संगठन पूंजीवादियों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं, तब इसके प्रति सन्तुलन के लिए मानववादी मुद्दों, पोषणकारी विकास तथा विकासशील देशों की सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों का उदय हुआ। कुछ महत्त्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन इस प्रकार हैं
(1) अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसायटी (International Red Cross Society):
अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसायटी एक महत्त्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्य कार्य युद्ध एवं संकट के समय असहाय लोगों की मदद करना है।
(2) एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International):
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अन्य महत्त्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार एवं प्रकाशित करवाता है।
(3) ह्यमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch):
ह्यमन राइट्स वॉच भी एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्य कार्य मानवाधिकारों की अवहेलना की ओर विश्वभर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करवाना है।

प्रश्न 3.
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर एक निबंध लिखिए।
उत्तर:
दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्तूबर, 1945 को अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र का प्रारंभिक सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अथवा संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 111 अनुच्छेद हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, नियमों, अंगों तथा इनकी शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का उल्लेख है।
संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य (Objectives of the United Nations):
संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में ही इस संगठन के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में एक आदर्श और गरिमामय विश्व समाज की स्थापना की बात कही गयी है। प्रस्तावना में कहा गया है कि, “हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को उस भावी-विश्व युद्ध से बचाएंगे जिसने हमारे जीवन काल में ही दो बार मानव जाति पर बहुत अधिक अत्याचार किए हैं। हम मनुष्यों के मूल अधिकारों, व्यक्ति के सम्मान और छोटे-बड़े सब राष्ट्र के नर-नारियों के समान अधिकारों में फिर से श्रद्धा बनाएंगे।
हम ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे जिससे न्याय स्थापित हो सके और अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों के लिए आदर की भावना बढ़ सके। हम अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे और समाज को प्रगतिशील बनाएंगे तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहिष्णुता और शान्तिपूर्वक अच्छे पड़ोसियों के समान रहने के लिए तथा इस बात को निश्चित करने के लिए कि सैनिक बल प्रयोग सामान्य हित के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर नहीं किया जाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय यन्त्र के सब जातियों को आर्थिक सामाजिक उन्नति में प्रयोग करने के लिए यह दृढ निश्चय करते हैं कि उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमेशा सहयोग प्रदान करेंगे।
इसलिए हमारी सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा-पत्र को स्वीकार किया है और हम एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध होगा।” चार्टर के अनुच्छेद एक में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन-समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्म-निर्णय के सिद्धान्त सम्बन्धी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानवतावादी स्वरूप पर आश्रित अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों को समन्वय करने के निमित्त एक केन्द्र का कार्य करना।
सानफ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति ने इसके चार उद्देश्य बतलाए
(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना तथा आक्रामक कार्यवाही को रोक कर शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना और शान्तिपूर्वक उपायों से उन विवादों का हल निकालना।
(2) विविध राष्ट्रों के बीच समान अधिकार, स्वाभिमान तथा जनता के आत्म-निर्णय के अधिकार के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना तथा विश्वशान्ति को सुदृढ़ करने के लिए विविध उपाय करना।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति करना तथा मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वाधीनता के अधिकार तथा जाति, रंग, भाषा, धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए प्रयास करना तथा इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
(4) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विविध राष्ट्रों के प्रयासों के बीच सामंजस्य की स्थापना के उद्देश्य से एक केन्द्र का कार्य करना। संयक्त राष्ट द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति-संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अत्यन्त आदर्शात्मक, व्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने वाले हैं।
लेकिन अपनी स्थापना से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई है। विशेष रूप से राजनीतिक विषयों पर तो संयुक्त राष्ट्र महाशक्तियों के द्वन्द्व का शिकार होकर रह गया है।महाशक्तियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए न तो संयुक्त राष्ट्र की कभी चिन्ता की और न अब कर रही है।
लेकिन गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की सफलता उल्लेखनीय रही है। बीमारियों को दूर करने, मानवाधिकारों की रक्षा, वैज्ञानिक शोध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास सराहनीय रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त-इसके लिए प्रश्न नं० 4 देखें।
प्रश्न 4.
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सिद्धान्तों की व्याख्या करो।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 में संघ के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। लेकिन उद्देश्यों का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। इनकी प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक था कि सदस्यों के मार्ग. दर्शन के लिए कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख चार्टर में किया जाता। अत: अनुच्छेद 2 में इन प्रमुख सिद्धान्तों की व्यवस्था । की गई है।
ये सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय आधार के उन नियमों की तरह हैं जो संयुक्त राष्ट्र और उनके सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अनुच्छेद 2 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघ और उसके सदस्य निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेंगे
(1) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सदस्य राष्ट्रों की प्रभुसत्ता की समानता के आधार पर की गई है।
(2) संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य ईमानदारी से घोषणा-पत्र के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करेंगे ताकि निर्धारित अधिकारों की प्राप्ति सभी को हो सके।
(3) संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य अपने विवादों का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग तथा इस प्रकार करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और न्याय को किसी प्रकार का भय न हो।
(4) सभी सदस्य राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता को आघात पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ ही वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र और उद्देश्यों के विपरीत या असंगत हो।
(5) संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अन्तर्गत लिए गए किसी कार्य के सन्दर्भ में सभी प्रकार की सहायता देंगे अर्थात् उस राष्ट्र की मदद नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कोई निरोधात्मक अथवा प्रतिरोधात्मक कार्यवाही कर रहा हो।
(6) विश्व-शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपेक्षित उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि वे सभी राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, घोषणा-पत्र के आधार पर आधारभूत सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।
(7) संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो उसके आन्तरिक हैं, न यह कोई भी कार्य करेगा, जिसको धमकी या दबाव कहा जा सके।
प्रश्न 5.
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं ? उनकी रचना तथा उनके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंर्गों का वर्णन करें।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुसार 6 मुख्य अंग हैं जिनके द्वारा संघ अपने बहुमुखी कर्तव्यों को पूरा करता है। ये अंग हैं-महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, ट्रस्टीशिप कौंसिल, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय . तथा सचिवालय। इन अंगों के संगठन, शक्तियों तथा कामों का विवरण नीचे दिया जा रहा है
1. महासभा (The General Assembly):
महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा तथा मुख्य चार्टर अंग है। यह एक प्रकार की विश्व संसद् है जिसका मुख्य काम विचार-विमर्श करना है। रचना (Composition) महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। इन 193 देशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर महासभा बनती है। हर सदस्य देश इसमें अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु हर देश का एक ही मत होता है। इसके कार्य तथा शक्तियां (Its power and Functions)-महासभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं
1. निर्वाचित कार्य-महासभा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों को दो साल के लिए चुनती है। महासभा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्य भी चुनती है। यह ट्रस्टीशिप कौंसिल के कुछ सदस्य चुनती है। सुरक्षा परिषद् तथा महासभा अलग-अलग मत प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों का चुनाव करती है। महासभा सुरक्षा परिषद् की सिफ़ारिश पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सचिव को नियुक्त करती है।
2. विचारशील कार्य-महासभा का सबसे महत्त्वपूर्ण काम चार्टर के अधीन सारे विषयों पर विचार करना तथा उसके आधार पर सिफ़ारिश करना है।
3. अन्य अंगों पर नियन्त्रण महासभा संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंगों एजेन्सियों पर नियन्त्रण करती है तथा उनके कार्यों का नियन्त्रण करती है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग महासभा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विचार करके सुझाव दे सकती है।
5. बजट-संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की ज़िम्मेदारी महासभा पर है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करती है, उसको पास करती है।
6. संशोधन कार्य-संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में महासभा 2/3 बहुमत से संशोधन करने की सिफ़ारिश कर सकती है।
2. सुरक्षा परिषद् (The Security Council):
सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है। चार्टर के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाने की ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद् पर है। रचना (Composition)-सुरक्षा परिषद् के कुल 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य दो प्रकार के होते हैं-स्थायी और अस्थायी। पांच सदस्य स्थायी हैं-ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी चीन। इसके 10 अस्थायी सदस्य दो वर्षों के लिए महासभा चुनती है।
वोट डालने की विधि (Voting Procedure)-सुरक्षा परिषद् में प्रत्येक सदस्य को एक मत डालने का अधिकार दिया गया है। सुरक्षा परिषद् में कार्य-विधि के मामलों (Procedural matters) में जैसे कार्य सूची (Agenda) को तैयार करने के लिए 15 में से कम-से-कम 9 सदस्यों के मत पक्ष में होने चाहिएं, परन्तु अन्य सभी मामलों के लिए 9 मतों में 5 बड़ी शक्तियों अर्थात् अमेरिका, साम्यवादी चीन, रूस, फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन के मत अवश्य ही शामिल होने चाहिएं।
सुरक्षा परिषद् के कार्य तथा शक्तियां (Functions and Powers of the Security Council):
संयुक्त राष्ट्र के अंगों में सुरक्षा परिषद् का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके मुख्य कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित हैं
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाए रखना,
- संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का चुनाव, 3 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन।
- आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (The Economic and Social Council)
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की स्थापना की गई है।
3. रचना (Composition):
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की सदस्य संख्या 54 है। ये सदस्य महासभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं और एक-तिहाई सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं। हर सदस्य देश को एक वोट का अधिकार होता है और इस परिषद् के निर्णय साधारण बहुमत से किये जाते हैं।
इसके कार्य (Its Functions) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के कार्यों का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 55 में किया गया है। सामाजिक-आर्थिक परिषद् सदस्य राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक सहयोग को बढ़ाने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण गतिविधियां संचालित करती है।
4. ट्रस्टीशिप कौंसिल (The Trusteeship Council) :
ट्रस्टीशिप कौंसिल जिसने लीग की मैंडेट प्रणाली का स्थान लिया है, का उद्देश्य पिछड़े हुए देशों का विकसित देशों के नेतृत्व में उन्नति दिलाना है ताकि वे शीघ्रता से स्वशासन के लिए तैयार हो सकें। इस प्रणाली के अधीन सुरक्षित प्रदेशों पर निगरानी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र-ट्रस्टीशिप कौंसिल की स्थापना की गई। यह परिषद् तीन प्रकार के प्रदेशों की निगरानी करती है
- वे प्रदेश, जो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए।
- वे प्रदेश, जो लीग के समय मैंडेट प्रणाली के अधीन थे।
- वे प्रदेश, जो अपनी मर्जी से इस प्रणाली के अधीन किए गए।
रचना (Composition) ट्रस्टीशिप कौंसिल में सुरक्षा परिषद् के सारे स्थाई सदस्य होते हैं। इनके अलावा सुरक्षित प्रदेशों का प्रबन्ध चलाने वाले देश भी इसके सदस्य होते हैं। इन दोनों तरह के कुल सदस्यों के बराबर महासभा इस परिषद् के लिए सदस्य चुनती है। इस परिषद् की साल में दो बैठकें होती हैं। इसके निर्णय बहुमत से होते हैं। इनके उद्देश्य तथा कार्य (Its Aims and Functions) ट्रस्टीशिप कौंसिल के चार मुख्य उद्देश्य हैं, जिनकी पूर्ति यह परिषद् करती हैं। वे अग्रलिखित हैं
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा में वृद्धि करना।
- सुरक्षित प्रदेशों का विकास करना ताकि वे स्वतन्त्रता के योग्य हो सकें।
- मौलिक मानवीय अधिकारों के लिए वातावरण बनाना।
- सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक विषयों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में समानता लाना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) :
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। रचना (Composition) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जज होते हैं जिन्हें महासभा तथा सरक्षा परिषद अलग-अलग स्वतन्त्र तौर पर चुनती है। जज 9 साल के लिए चुने जाते हैं। एक-तिहाई न्यायाधीश अर्थात् पांच जज हर तीन वर्ष बाद रिटायर होते हैं और उनकी जगह 5 जज चुन लिये जाते हैं।
इसका क्षेत्राधिकार (Its Jurisdiction)-अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों से सम्बन्धित सभी विषय इसके पास ले जाए जा सकते हैं। इस न्यायालय में केवल राज्यों के झगड़े ही ले जाए जा सकते हैं, व्यक्तियों के नहीं। इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है
- अनिवार्य क्षेत्राधिकार,
- ऐच्छिक क्षेत्राधिकार,
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
6. सचिवालय (The Secretariat):
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबन्धक काम चलाने के लिए चार्टर के अनुसार सचिवालय स्थापित किया गया है, जिसमें संगठन की ज़रूरत अनुसार कर्मचारी होते हैं जिनका मुखिया महासचिव होता है। महासचिव जिसे संसार का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कहा जा सकता है, सुरक्षा परिषद् की सिफ़ारिश पर महासभा नियुक्त करती है। यह 5 साल के लिए चुना जाता है।
सचिवालय के 9 विभाग है और हर भाग का मुखिया उप-महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में दुनिया के अनेक देशों के नागरिक काम करते हैं, किन्तु उन सबकी वफ़ादारी विश्व संस्था के प्रति होती है। सचिवालय के अधिकारियों के लिए स्वतन्त्र रूप से अपने कार्यों को करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की कार्यवाहियों को लिखता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को प्रकाशित करता है।
प्रश्न 6.
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर एक लेख लिखें।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाने के लिए 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के आरम्भ में 51 सदस्य थे और वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। भारत संयुक्त राष्ट्र का प्रारम्भिक सदस्य है और इसे विश्व-शान्ति के लिए महत्त्वपूर्ण संस्था मानता है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के योगदान का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है
1. भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना-भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारम्भिक सदस्य बन गया। सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि श्री ए. रामास्वामी मुदालियर ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय का महत्त्व सर्वाधिक होना चाहिए। भारत की सिफ़ारिश पर चार्टर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करने का उद्देश्य जोड़ा गया।
2. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बढ़ाने में भारत की भूमिका-भारत की सदा ही यह नीति रही है कि विश्व शान्ति को बनाए रखने के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए संसार के सभी देशों को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं, सदस्य बनना चाहिए। इसलिए 1950 से लेकर अगले 20 वर्षों तक लगातार जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन को सदस्य बनाने का प्रश्न आया, भारत ने सदैव इसका समर्थन किया।
परन्तु अमेरिका सुरक्षा परिषद् में चीन की सदस्यता के प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग करता रहा। 1972 में अमेरिका के चीन के प्रति दृष्टिकोण बदलने पर ही चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत ने बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में भारत का स्थान-संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों और विशेष एजेन्सियों में भारत को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। 1954 में भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित महासभा (General Assembly) की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। 1956 में स्वर्गीय डॉ० राधाकृष्ण यूनेस्को के प्रधान चुने गये।
भारत आठ बार सुरक्षा परिषद् का सदस्य रह चुका है और 30 सितम्बर, 1991 को भारत ने सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष का कार्यभार एक महीने के लिए सम्भाला। सामाजिक और आर्थिक परिषद् का भारत लगभग निरन्तर सदस्य चला आ रहा है। भारत के डॉ० नगेन्द्र सिंह को 1973 और 1982 में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया था। फिर फरवरी, 1985 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। 1989 में भारत के आर० एस० पाठक को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया।
जनवरी, 2003 में प्रथम भारतीय महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त हुई। वे इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली न केवल प्रथम भारतीय अपितु विश्व की प्रथम महिला अधिकारी भी हैं। 27 अप्रैल, 2012 को न्यायमूर्ति दलवीर भण्डारी को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया। नवम्बर, 2017 में दलवीर भण्डारी को पुनः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुन लिया गया।
4. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से भारत का योगदान-संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। भारत में विश्व-शान्ति सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं
(i) कोरिया की समस्या-1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध को रोकने के लिए 16 राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी कोरिया के प्रतिरोध के लिए भेजीं। भारत के सैनिकों ने भी इस कार्यवाही में भाग लिया। भारत ने इस युद्ध को समाप्त कराने तथा युद्धबन्दियों का आदान-प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को तटस्थ राष्ट्र आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
(ii) स्वेज नहर की समस्या-जुलाई, 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीकरण कर दिया। इस पर इंग्लैण्ड, फ्रांस और इज़राइल ने मिलकर मित्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इन देशों की निन्दा की और महासभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें यह कहा गया कि युद्ध को तुरन्त बन्द कर दिया जाए। स्वेज नहर समस्या को हल करने में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
(iii) कांगो समस्या-स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर कांगो में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए बैल्जियम ने कांगो में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लुमुम्बा ने संयुक्त राष्ट्र से सैनिक सहायता की अपील की। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील पर भारत ने अपनी सेना कांगो भेजी। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सेना में सबसे बड़ी टुकड़ी भारतीय बटालियन की थी।
(iv) अरब-इजराइल विवाद-1967 में अरब-इज़राइल युद्ध में इज़राइल ने अरब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत की नीति यह रही है कि इज़राइल को अरब क्षेत्र खाली करने चाहिएं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को मानना चाहिए।
(v) अफ़गानिस्तान की समस्या-अफ़गानिस्तान की समस्या हल करने में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
(vi) खाड़ी युद्ध-भारत ने फरवरी, 1991 को खाड़ी युद्ध में गैर-सैनिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की तुरन्त बैठक बुलाकर खाड़ी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने की मांग की। सुरक्षा परिषद् में पूरी स्थिति की समीक्षा कर यह देखा कि खाड़ी में अमेरिका और बहुराष्ट्रीय देशों की सैनिक कार्रवाई सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 678 के अनुसार है या नहीं। उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भारत ने अन्य समस्याओं को सुलझाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5. उपनिवेशवाद का विरोध-भारत उपनिवेशवाद का सदा ही विरोधी रहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज बुलन्द की। बंगला देश को स्वतन्त्र करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दिलाने का प्रयत्न किया है, भारत ने इसका समर्थन किया है।
6. रंग-भेद के विरुद्ध संघर्ष- भारत ने रंग-भेद की नीति को विश्व-शान्ति के लिए खतरा माना है। रंग-भेद पक्षपात का सबसे व्यापक अभ्यास तथा भ्रष्टपूर्ण प्रदर्शित उदाहरण एशिया तथा अफ्रीका के काले वर्गों के प्रति गोरों की धारणा थी। रंग-भेद नीति में दक्षिण अफ्रीकी सरकार सबसे आगे रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कई बार रंग-भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई और विश्व जनमत तैयार किया, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक प्रस्ताव पारित किए।

7. निःशस्त्रीकरण के प्रयासों में भारत का सहयोग-संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों के ऊपर यह जिम्मेवारी डाली गई है कि वे निःशस्त्रीकरण के लिए कार्य करें। भारत की नीति यही है कि निःशस्त्रीकरण के द्वारा ही विश्व-शान्ति को बनाए रखा जा सकता है और अणु शक्ति का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। भारत पूर्ण निःशस्त्रीकरण के पक्ष में है और उसने संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है।
8. मानव अधिकारों की रक्षा-भारत मानव अधिकारों का महान् समर्थक है। भारत ने अपने नागरिकों को लगभग वे सभी अधिकार दिए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए हैं। जब भी किसी देश ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उसके विरुद्ध आवाज उठाई और संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही की।
9. गट-निरपेक्ष आन्दोलन-भारत गट-निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक है और इस आन्दोलन ने शीत यद्ध को कम किया है और संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह दो गुटों में विभक्त होने से बचाया है।
10. आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने में भारत की भूमिका-भारत का सदा यह विचार रहा है कि विश्व-शान्ति की स्थायी स्थापना तभी हो सकती है, यदि आर्थिक और सामाजिक अन्याय को समाप्त किया जाए। भारत ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत ने आर्थिक दशा से पिछड़े देशों के विकास पर विशेष बल दिया है और विकसित देशों को अविकसित देशों की अधिक-से-अधिक सहायता करने के लिए कहा है।
11. पर्यावरण की रक्षा-पर्यावरण का प्रदषण मानवता के लिए खतरा बन गया है। संसार के जीवनदायी वन एवं नदियां ही नहीं, धरती, वनस्पतियां और विश्व महासागर भी प्रदूषण की चपेट में आते जा रहे हैं। प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने कई बार कहा था कि विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं।
12. संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली सुधारने में भारत की भूमिका-1 फरवरी, 1992 को सुरक्षा परिषद् की शिखर बैठक हुई ताकि सुरक्षा परिषद् को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। भारत के प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव ने 15 – सदस्यीय सुरक्षा परिषद् के विस्तार और विश्व के सबसे बड़े संगठन को और अधिक लोकतान्त्रिकरण पर जोर दिया।
संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्वगठन और सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों में विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। निष्कर्ष-भारत विश्व-शान्ति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग देता है और भारत का अटल विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व-शान्ति को बनाए रखने का महत्त्वपूर्ण यन्त्र है।
प्रश्न 7.
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए कुछ सुझाव दीजिए।
अथवा
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार के लिये सुझाव दीजिये।
उत्तर:
सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद् को सौंप दिया गया है। यद्यपि सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है, तथापि इसमें कुछ कमियां हैं, जिनमें सुधारों की मांग समय-समय पर उठती रहती है। निम्नलिखित कारणों से सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग की जाती रही है
1. संयुक्त राष्ट्र की बढ़ती हुई सदस्य संख्या-सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग करने वाले राष्ट्रों, जिनमें भारत भी शामिल है, का कहना है कि जिस अनुपात में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद् में सदस्य राष्ट्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। अत: सुरक्षा परिषद् को अधिक लोकतान्त्रिक बनाने के लिए सुरक्षा परिषद् में सदस्यों की संख्या, विशेषकर स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
2. नई चुनौतियां-विश्व में उभर रही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग चल रही है।
3. असमान प्रभुसत्ता-सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थाई सदस्य हैं, जिन्हें वीटो (Veto) प्राप्त है, जबकि 10 अस्थाई सदस्य हैं। इससे पता चलता है कि सुरक्षा परिषद् में समानता के अधिकार को मान्यता न देकर असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व पाया जाता है, अतः कई सदस्य राष्ट्र इस भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं।
4. वीटो की समस्या-वीटो की समस्या को समाप्त करने के लिए भी सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग की जा रही है।
5. महाशक्तियों के प्रभत्व को कम करना-सरक्षा परिषद में 5 सदस्य राष्ट्रों (अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस और चीन) को वीटो शक्ति दी गई है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गये हैं, अतः उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए भी सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग की जा रही है।
सुरक्षा परिषद् में किए जाने वाले सुधार
1. सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए-सुधारों की मांग करने वाले सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसे अधिक लोकतान्त्रिक बनाने की मांग कर रहे हैं। विशेषकर स्थाई सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी की मांग जोर पकड़ती जा रही है।
2. वीटो की समाप्ति-सुरक्षा परिषद् की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक बनाने के लिए या तो वीटो की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए, या फिर इसे सीमित कर देना चाहिए।
3. समान सदस्यता-सुरक्षा परिषद् में अस्थाई सदस्यों की धारणा को समाप्त करके सबको समान स्तर की सदस्यता प्रदान करनी चाहिए।
4. सुरक्षा परिषद् को महासभा के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जाए-सुरक्षा परिषद् में सुधारों की मांग करने वालों का कहना है कि यदि सुरक्षा परिषद् को विश्व के लोगों का विश्वास जीतना है, तो इसे महासभा के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
5. सामाजिक और आर्थिक कार्य सुरक्षा परिषद् को दिए जाने की मांग-कई विचारक कहते हैं कि सुरक्षा परिषद् को केवल राजनीतिक कार्य ही दिये जाते हैं जिससे इसके सदस्यों में सदैव मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, अतः इनमें सहयोग उत्पन्न करने के लिए सुरक्षा परिषद् को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिये जाने चाहिएं।
प्रश्न 8.
एक विश्व संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं और असफलताओं पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1945 से लेकर अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल किया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शान्ति को बनाए रखने, युद्धों को रोकने तथा महाशक्तियों में टकराव को रोकने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र को जहां अनेक सफलताएं प्राप्त हुई हैं वहीं इसे असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की सफलताओं एवं असफलताओं का वर्णन इस प्रकार है
1. राजनीतिक उपलब्धियां-संयुक्त राष्ट्र ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ विवाद इस प्रकार हैं-रूस-ईरान विवाद, यूनान विवाद, सीरिया और लेबनान की समस्या, इण्डोनेशिया की समस्या कोर्फ़ चैनल विवाद, कोरिया समस्या, स्वेज़ नहर की समस्या, कांगो समस्या, यमन विवाद, कुवैत-ईराक विवाद आदि।
2. निःशस्त्रीकरण-संयक्त राष्ट्र ने नि:शस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने नि:शस्त्रीकरण के लिए अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया है।
3. अन्तरिक्ष का मानव कल्याण के लिए प्रयोग-संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप ही महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि बाहरी अन्तरिक्ष का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा।
4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है।
5. अन्य उपलब्धियां-संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक इत्यादि गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र की असफलताएं-संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित मामलों में असफलताओं का मुंह देखना पड़ा है
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य युद्धों को रोकना और विश्व में शान्ति स्थापित करना है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र इस उद्देश्य में पूर्णरूप से सफल नहीं हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र अनेक राजनीतिक तथा अन्य झगड़ों को दूर करने में असफल रहा है।
- नि:शस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की कोई महान् उपलब्धि नहीं रही है।
- दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद की नीति के विषय में संयुक्त राष्ट्र कारगर नहीं रहा।
- मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा सका।
- महाशक्तियों की मनमानी रोकने में संयुक्त राष्ट्र बुरी तरह से असफल रहा है।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र कब स्थापित हुआ? क्या भारत इसका मूल रूप से सदस्य है ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना संविधान है जिसे चार्टर (Charter) कहा जाता है और यह चार्टर सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय अमेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयार्क में स्थित है।
आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्य थे, परन्तु आजकल इसकी सदस्य संख्या 193 है। भारत इसके आरम्भिक सदस्यों में से है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्म निर्णय के सिद्धान्त पर आश्रित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना और इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों को चलाने के लिए एक केन्द्र का कार्य करना है।

प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के किन्हीं चार उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करें।
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना है तथा युद्धों को रोकना और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा हल करना है।
- भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच समान अधिकारों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना है।
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति करना।
- मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के लिए सम्मान बढ़ाना।
प्रश्न 3.
भारत की संयुक्त राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अंगों में क्या भूमिका रही है ?
उत्तर:
भारत अनेक बार संयुक्त राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है, जैसे कि
- भारत सुरक्षा परिषद् का आठ बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत ने सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत सामाजिक तथा आर्थिक परिषद् का सदस्य अनेक बार रह चुका है और अब पिछले कुछ वर्षों से भारत इस परिषद् का निरन्तर सदस्य चला आ रहा है।
- 1956 में भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित महासभा की अध्यक्षा चुनी गई।
- 1956 ई० में राधाकृष्णन यूनेस्को के अध्यक्ष चुने गए।
- सर बेनेगल राव 1950 के दशक में अन्तर्राष्टीय न्यायालय के जज रह चके हैं।
डॉ० नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय य के न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त श्री रामस्वरूप पाठक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 27 अप्रैल, 2012 को न्यायमूर्ति दलवीर भण्डारी को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया। नवम्बर, 2017 में दलवीर भण्डारी को पुन: अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुन लिया गया।
प्रश्न 4.
सुरक्षा परिषद् पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।
उत्तर:
सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के समान है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं- स्थायी और अस्थायी। पांच स्थायी सदस्य हैं-अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य दो वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद् में रखे गए प्रस्ताव के विरोध में अपना मत देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता।
उल्लेखनीय है कि यदि कोई सदस्य विरोध स्वरूप सुरक्षा परिषद् की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं माना जाता। सुरक्षा परिषद् का प्रमुख कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद् नए सदस्यों को महासभा की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाती है। इसके अलावा यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों व महासचिव के चुनाव में भी भाग लेती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन के विषय में भी सुरक्षा परिषद् महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
प्रश्न 5.
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कोई चार कार्य लिखिये।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के महासचिव के कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र का एक सचिवालय होता है जिसका मुखिया महासचिव होता है। महासचिव जिसे विश्व का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कहा जा सकता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफ़ारिश पर महासभा करती है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस समय श्री एन्टोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं।
(1) महासचिव सचिवालय के सभी कर्मचारियों पर निरीक्षण रखता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(2) यह महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक व सामाजिक परिषद्, ट्रस्टीशिप कौंसिल की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है।
(3) यह महासभा के सामने संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है।
(4) महासचिव सुरक्षा परिषद् का ध्यान किसी ऐसे विषय की ओर दिलाने का कार्य भी करता है जो अन्तर्राष्टीय शांति एवं सरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। महासचिव का अन्तर्राष्टीय शांति बनाने रखने में बड़ा हाथ होता है।
प्रश्न 6.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय पर एक टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का हल करने के लिए हेग में एक न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया गया है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव महासभा तथा सुरक्षा सुरक्षा परिषद् द्वारा अलग अलग स्वतन्त्र तौर पर किया जाता है। न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों से सम्बन्धित सभी विषय ले जाए जा सकते हैं। इस न्यायालय में केवल राज्यों के ही झगड़े ले जाए जा सकते हैं, व्यक्तियों के नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का है
- अनिवार्य क्षेत्राधिकार
- ऐच्छिक क्षेत्राधिकार
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संधियों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को भंग करने वाले तथ्यों व क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित पक्षों को सुनता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्बन्धित राज्यों की सहमति से ही किसी अभियोग की सुनवाई करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद् को आवश्यकतानुसार किसी मामले में सलाह भी दे सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रश्न 7.
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) में भारत की भूमिका का वर्णन करें।
उत्तर:
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए 1945 में सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह संयुक्त राष्ट्र का प्रारम्भिक सदस्य बन गया। भारत की सिफारिश पर चार्टर में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करने का उद्देश्य जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों और विशेष एजेन्सियों में भारत को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। भारत सुरक्षा परिषद् का आठ बार अस्थायी सदस्य रह चुका है।
भारत ने विश्व शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी संसार में किसी भी भाग में तनाव या झगड़ा उत्पन्न हुआ है तो भारत ने तनाव को कम करने तथा झगड़े को हल करने के प्रयास किए हैं। कोरिया, स्वेज़ नहर, कांगो, साइप्रस, अलजीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान आदि की समस्याओं को हल करने में भारत ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जब कभी सुरक्षा परिषद् ने किसी देश में शान्ति स्थापित करने के लिए सेनाओं की मांग की तो भारत ने अपनी सेनाएं भेजी हैं।

प्रश्न 8.
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की दृष्टि से भारत के योगदान की चर्चा करो।
अथवा
भारत ने विश्व शान्ति की स्थापना में क्या भूमिका अभिनीत की है ?
उत्तर:
भारत ने विश्व-शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है
1. कोरिया समस्या-1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध को रोकने के लिए 16 राष्ट्रों की सेनाएं उत्तरी कोरिया के विरुद्ध भेजी। भारत के सैनिकों ने भी इस कार्यवाही में भाग लिया।
2. स्वेज नहर की समस्या-जुलाई, 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस पर इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा इज़राइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इन देशों की निन्दा की और महासभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि युद्ध को तुरन्त बन्द कर दिया जाए।
3. कांगो समस्या-स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर कांगो में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। लुमुम्बा ने संयुक्त राष्ट्र से सैनिक सहायता की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की अपील पर भारत ने अपनी सेना कांगो में भेजी।।
4. अरब-इजराइल विवाद-1967 में अरब-इज़राइल युद्ध में इज़राइल ने अरब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत की नीति यह रही है कि इज़राइल को अरब क्षेत्र खाली करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित सभी प्रस्तावों को मानना चाहिए।
प्रश्न 9.
संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र के कोई चार सिद्धांत लिखिए।
उत्तर:
(1) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सदस्य राष्ट्रों की प्रभुसत्ता की समानता के आधार पर की गई है।
(2) संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य ईमानदारी से घोषणा-पत्र के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करेंगे ताकि निर्धारित अधिकारों की प्राप्ति सभी को हो सके।
(3) संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग तथा इस प्रकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को किसी प्रकार का भय न हो।
(4) सभी सदस्य राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता को आघात पहुंचाने वाला कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ ही वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र और उद्देश्यों के विपरीत या असंगत हो।
प्रश्न 10.
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने के लिए चार सुझाव दीजिए।
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रासंगिक सुधार करना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- विश्व शान्ति को बढ़ावा देने के लिए एक शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए।
- विश्व में व्याप्त किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा एवं उसे नियन्त्रित करना।
प्रश्न 11.
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संघ (UNESCO) पर एक नोट लिखें।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन जिसे प्रायः यूनेस्को के नाम से पुकारा जाता है, ने राष्ट्र संघ के अधीन बनाई गई अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों के सहयोगी संगठन का स्थान लिया है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवम्बर, 1946 की गई। इनकी स्थापना के लिए लन्दन में 1 नवम्बर से 16 नवम्बर, 1945 तक एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सम्मेलन की कार्यवाही बड़ी उत्साहपूर्ण वातावरण में चली। विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया। इंग्लैंड तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस संगठन के संविधान का निर्माण किया। लगभग एक वर्ष के बाद संविधान के स्वीकृत होने पर यूनेस्को की 4 नवम्बर, 1946 को विधिवत् स्थापना की गई। समझौते द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने इस संगठन को अपने विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्वीकार कर लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का प्रचार-प्रसार करना है।
प्रश्न 12.
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कोई चार विशेषताएँ लिखें।
उत्तर:
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों का एक संगठन होता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में सभी सदस्य राज्यों को समान समझा जाता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का संचालन स्थायी अभिकरणों एवं प्रक्रियाओं द्वारा चलाया जाता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना सदस्य राज्यों द्वारा अपने सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए होती है।
प्रश्न 13.
भारत के सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यता के दावे को मजबूत करने वाले दो कारण बताएं।
उत्तर:
1. विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश-भारत के सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यता के दावे का प्रमुख कारण यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक एवं जिम्मेदार देश है। भारत में नियमित समय पर चुनाव होते हैं तथा सभी लोगों को समान रूप से मताधिकार प्राप्त हैं।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका-भारत के सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यता के दावे का एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई है तथा विश्व में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सदैव सहयोग दिया है।
प्रश्न 14.
एक ध्रुवीय युग में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की आवश्यकता के कोई चार कारण लिखिए।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता के कोई चार कारण लिखिये।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित कारणों से एक अपरिहार्य संगठन हैं
1. विश्व में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है। विश्व में बढ़ते आतंकवाद एवं भय को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की ही आवश्यकता है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है।
3. मानवाधिकार की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है।
4. निःशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है।
प्रश्न 15.
भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?
उत्तर:
भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं
- भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व बैंक ने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञ एवं ऋण उपलब्ध करवाया है।
- यूनेस्को ने भारत में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कई क्षेत्रों को कृषि युक्त बनाने का प्रयास किया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कई प्रकार की बीमारियों को रोकने एवं समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रश्न 16.
सुरक्षा परिषद् के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए किन्हीं चार मानदण्डों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
- सुरक्षा परिषद् में उन नये देशों को शामिल किया जाए, जिनका मानवाधिकारों से सम्बन्धित रिकॉर्ड अच्छा है।
- सुरक्षा परिषद् में नये सदस्यों को शामिल करने का एक अन्य मानदण्ड भूगोलिक आधार है।
- आर्थिक आधार पर भी सुरक्षा परिषद् की सदस्यता बढ़ाये जाने का सुझाव दिया जा रहा है।
- कुछ विद्वानों का विचार है कि उन देशों को सुरक्षा परिषद् में शामिल किया जाए जिन्होंने विश्व शांति स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रश्न 17.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन एवं कार्य लिखें।
उत्तर:
महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा मुख्य चार्टर अंग है। यह एक प्रकार की विश्व संसद् है जिसका मुख्य काम विचार-विमर्श करना है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। इन 193 देशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर महासभा बनती है। हर सदस्य देश इसमें अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परन्तु हर देश का एक ही मत होता है।
1. निर्वाचित कार्य-महासभा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों को दो साल के लिए चुनती है। महासभा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्य भी चुनती है। यह ट्रस्टीशिप कौंसिल के कुछ सदस्य चुनती है। सुरक्षा परिषद् तथा महासभा अलग-अलग मत प्रयोग करके अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जजों का चुनाव करती है। महासभा सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सचिव को नियुक्त करती है।।
2. विचारशील कार्य-महासभा का सबसे महत्त्वपूर्ण काम चार्टर के अधीन सारे विषयों पर विचार करना तथा उसके आधार पर सिफ़ारिश करना है।
प्रश्न 18.
राष्ट्र संघ की असफलता के कोई चार कारण बताएं।
उत्तर:
राष्ट्र संघ की असफलता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं
- राष्ट्र संघ में विभिन्न देशों को असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त था।
- राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं थी।
- राष्ट्र संघ में ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे बड़े देशों का प्रभाव अधिक था, जबकि कमज़ोर देशों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था।
- राष्ट्र संघ की असफलता के लिए सदस्य देशों की अव्यावहारिक नीतियां भी ज़िम्मेदार हैं।
प्रश्न 19.
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद् किन चार तरीकों का प्रयोग करती है ?
उत्तर:
1. वार्ता-इससे अभिप्राय है कि दो राष्ट्रों में अपने विवाद का समाधान करने हेतु बातचीत करना। बातचीत राष्ट्रों के मध्य भी हो सकती है और ऐसी बातचीत उनके प्रतिनिधियों के मध्य भी हो सकती है।
2. सत्सेवा और मध्यस्थता-यदि सम्बद्ध दोनों पक्षों में वार्ता का ढंग अपनाने पर समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता तो अन्य देशों द्वारा उस विवाद के समाधान के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
3. वाद-विवाद-यह विधि महासभा या सुरक्षा परिषद् द्वारा ग्रहण की जाती है। महासभा या सुरक्षा परिषद् द्वारा विवादग्रस्त दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपने तर्क एवं दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार दोनों विरोधी ‘पक्षों को बिना किसी भय के अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच मिल जाता है और वाद-विवाद के माध्यम से विवाद के समाधान की आशा बढ़ जाती है।
4. जांच-इस विधि में विवाद के तथ्यों की जांच की जाती है। इस जांच द्वारा उन वास्तविकताओं का पता लगाया जाता है जिनसे विवादी पक्षों के मतभेदों को समाप्त किया जा सके।
प्रश्न 20.
शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् विश्व में हुए ऐसे कोई चार परिवर्तन लिखें जिनसे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावित हुआ है ?
उत्तर:
- 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया।
- पिछले कुछ वर्षों में चीन ने उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
- 9/11 की आतंकवादी घटना ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावित किया है।
- विश्व में एड्स, आतंकवाद, जनसंहार, परमाणु हथियार, पर्यावरण क्षरण, वैश्विक तापन, महामारी तथा गृह युद्ध जैसी समस्याएं संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावित कर रही हैं।
प्रश्न 21.
विश्व बैंक के किन्हीं चार कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
विश्व बैंक निम्नलिखित कार्य करता है
- विश्व बैंक मानवीय विकास से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।
- विश्व बैंक विश्व स्तर आधारभूत ढांचा तैयार करवाने में अपनी भूमिका निभाता है।
- विश्व बैंक सदस्य देशों को अनुदान एवं ऋण प्रदान करता है।
- विश्व बैंक अधिक ग़रीब देशों को अनुदान या ऋण देकर उन्हें वापिस नहीं लेता।
प्रश्न 22.
सितम्बर, 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावशाली एवं प्रांसगिक बनाने के लिए पास किए गए कोई चार प्रस्ताव लिखें।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) में सुधार के कोई चार सुझाव दीजिये।
उत्तर:
- विश्व शान्ति को बढ़ावा देने के लिए एक शान्ति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए।
- विश्व में व्याप्त किसी भी प्रकार के आंतकवाद की निन्दा एवं उसे नियन्त्रित करना।
- एक लोकतान्त्रिक कोष का गठन करना।
- यदि कोई देश अपने नागरिकों की रक्षा में सक्षम नहीं है, तो विश्व समुदाय को उसकी रक्षा करनी चाहिए।
प्रश्न 23.
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की सुरक्षा परिषद् के कार्यों का वर्णन कीजिए।
अथवा
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् के किन्हीं चार कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
सुरक्षा-परिषद् के निम्नलिखित कार्य हैं
(1) सुरक्षा परिषद् किसी ऐसे मामले पर तुरन्त विचार कर सकती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के भंग होने का भय हो।
(2) सुरक्षा-परिषद् आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शान्ति के लिए खतरे की सम्भावनाओं और शान्ति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकता है।
(3) सुरक्षा परिषद् प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
(4) चार्टर के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं, उन्हें निभाने की ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद् की है।
प्रश्न 24.
विश्व व्यापार संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यह संगठन ‘जेनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ’ के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 161 है। यह संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निश्चित करता है। इस संगठन में प्रत्येक निर्णय सदस्य देशों की सहमति पर लिया जाता है।
यद्यपि यह संगठन विश्व स्तर पर व्यापारिक नियमों को निश्चित करता है, परन्तु फिर भी इस पर अमेरिका, यूरोपीय देशों तथा जापान जैसे देशों का प्रभाव अधिक है, जोकि अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इस संगठन का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए विकासशील देश इस संगठन की कार्यप्रणाली से सन्तुष्ट नहीं रहते। विकासशील देशों का यहां आरोप है कि विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है तथा यह संगठन बड़ी शक्तियों के प्रभाव में कार्य करता है।
प्रश्न 25.
ह्यूमन राइट वॉच के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
- ह्यूमन राइट वॉच विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाला एक स्वयं सेवी संगठन है।
- ह्यूमन राइट वॉच मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर विश्व मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है।
- ह्यूमन राइट वॉच ने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने का प्रयास किया है।
- ह्यूमन राइट वॉच बाल सैनिकों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है।।

प्रश्न 26.
विश्व के किन्हीं चार प्रमख अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का वर्णन करें।
उत्तर:
- विश्व व्यापार संगठन-विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन् 1995 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों के विषय में नियम बनाने के लिए की गई थी।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है।
- गैट समझौता-गट समझौते का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों को समान रूप से भागीदार बनाना है।
- विश्व बैंक-विश्व बैंक की स्थापना सन् 1946 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता देना है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ?
अथवा
संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था ?
उत्तर:
द्वितीय विश्वयुद्ध की भयानक तबाही देखकर संसार के सभी भागों में प्रत्येक मनुष्य सोचने लगा कि यदि ऐसा एक और युद्ध हुआ तो विश्व तथा मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाने लगे। इसके लिए किसी विश्व समुदाय का होना ज़रूरी था।
अत: 24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के लिए राष्ट्रों के कार्यों को समन्वय करने के लिए एक केन्द्र का कार्य करना है। आरम्भ में उसके 51 राष्ट्र सदस्य थे और वर्तमान में इसके 193 राष्ट्र सदस्य हैं।
प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में वीटो’ शक्ति का प्रयोग करने वाले देशों के नाम बताइये।
उत्तर:
सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद् की कुल सदस्य संख्या 15 है। इनमें 10 अस्थायी सदस्य हैं तथा 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद् में वीटो अधिकार प्राप्त है। ये देश हैं-अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस तथा चीन।
प्रश्न 3.
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा करती है। महासचिव के लिए उम्मीदवार का नाम सुरक्षा परिषद् के 9 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इन नौ सदस्यों में से पांच सदस्य राजनीतिक विज्ञान ( स्थायी होने चाहिए।
यदि पांच स्थायी सदस्यों में से एक स्थायी सदस्य भी निषेधाधिकार का प्रयोग कर दे तो महासचिव के पद के नामांकित व्यक्ति का नाम निरस्त हो जाता है। सुरक्षा परिषद् द्वारा नामित उम्मीदवार को महासभा में उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। बहुमत प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुन लिया जाता है।
प्रश्न 4.
संयुक्त राष्ट्र की चार विशिष्ट एजेन्सियों (Specialised Agencies) के नाम लिखो।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र की चार विशिष्ट एजेन्सियों के नाम इस प्रकार हैं
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन।
- खाद्य एवं कृषि संगठन।
प्रश्न 5.
निषेधाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।
उत्तर:
निषेधाधिकार या वीटो सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की महत्त्वपूर्ण शक्ति है। निषेधाधिकार का अर्थ है स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकना। इसका अभिप्राय यह है कि यदि पांच स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में रखे गए प्रस्ताव के विरोध में वोट डाल दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद् में यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं माना जाएगा।
- प्रश्न 6.
संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) के कोई दो उद्देश्य बताइए।
उत्तर: - संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना है तथा युद्धों को रोकना और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा हल करना है।
- भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच समान अधिकारों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना है।
प्रश्न 7.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के कोई दो कार्य लिखें।
उत्तर:
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं
- दवाओं और स्वास्थ्य से सम्बद्ध वस्तुओं के लिए उचित मानक (Standard) निर्धारित करना।
- स्वास्थ्य के लिए प्रशासकीय नियमों का अध्ययन करके उनमें सुधारार्थ प्रयास करना।
प्रश्न 8.
हमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कोई दो कारण बताइए।
उत्तर:
- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शान्ति के विषयों में मदद करते हैं।
- राष्ट्रों के समक्ष कई बार ऐसी मुश्किल एवं बड़ी समस्या आ जाती है कि वे अकेला उसका हल नहीं निकाल सकता। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है।
प्रश्न 9.
संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) के कोई दो सिद्धान्त बताइए।
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संप्रभु समानता पर आधारित है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ईमानदारी से घोषणा-पत्र के अन्तर्गत निर्धारित दायित्वों का पालन करेंगे।
प्रश्न 10.
उन भारतीय अधिकारियों के नाम लिखो जो संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे हैं।
उत्तर:
- 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित महासभा की अध्यक्ष चुनी गई।
- डॉ० राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कमाल आजाद यूनेस्को के अध्यक्ष चुने गए।
- राजकुमारी अमृतकौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष चुनी गई थी।
- 1956 में श्री वी० आर० सेठ खाद्य और कृषि संगठन के अध्यक्ष चुने गए थे।
- डॉ० नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे।
प्रश्न 11.
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में भारत की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945 को की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और चार्टर पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र का प्रारम्भिक सदस्य बना। सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि श्री ए. रामास्वामी मुदालियर ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को रोकने के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय का महत्त्व सर्वाधिक होना चाहिए। भारत की सिफ़ारिश पर चार्टर में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहन करने का उद्देश्य जोड़ा गया।
प्रश्न 12.
संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन से अभिप्राय इस संगठन में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव करने से है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व राजनीति में बहुत बदलाव आए हैं और बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं कार्यप्रणाली में कुछ दोष उत्पन्न हो गए हैं, जिससे कारण समय-समय इसके पुनर्गठन की मांग की जाती है।

प्रश्न 13.
संयुक्त राष्ट्र संघ के किन दो महत्त्वपूर्ण अंगों में सुधार की मांग की जा रही है ?
उत्तर:
1. सुरक्षा परिषद्-संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में सुधार की सबसे अधिक मांग की जा रही है। क्योंकि इसमें सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता।
2. महासभा-संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भी समय-समय पर सुधार की मांग ली जाती रही है। भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के अनुसार महासभा में सर्वसम्मति की प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए तथा महासभा अध्यक्ष को आर्थिक शक्तिशाली बनना चाहिए।
प्रश्न 14.
संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन में भारत की स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता का एक मजबूत उम्मीदवार है। नई मानवाधिकार परिषद् के 47 सदस्यों में से एक भारत भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सुधारों तथा इसकी स्थाई सेना की धारणा में भी भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
प्रश्न 15.
वैश्विक तापवृद्धि (Global Warming) का क्या अर्थ है ?
उत्तर:
वैश्विक तापवृद्धि से अभिप्राय कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ने से है। वैश्विक तापवृद्धि क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक तापवृद्धि से समुद्री तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ गया है क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है।
प्रश्न 16.
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई दो कार्य बताएं।
उत्तर:
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विश्व स्तर पर वित्त व्यवस्था को नियन्त्रित करता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों की अपील पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
प्रश्न 17.
विश्व को संयुक्त राज्य अमेरिका से क्यों डर लगता है ? कोई दो कारण बताएं।
उत्तर:
- शीत युद्ध की समाप्ति एवं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया है।
- अमेरिका को अपनी इच्छानुसार कार्य करने से कोई देश या संगठन रोकने में सक्षम नहीं है।
प्रश्न 18.
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह का वर्णन करें।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व संस्था है। अत: संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, तथा इसे चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं जोकि विश्व शान्ति का सन्देश देती हैं।
प्रश्न 19.
भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है ?
उत्तर:
भारत अब तक आठ बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत सन् 1950, 1967, 1977, 1972, 1984, छठी बार 1991 में सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत सातवीं बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 तथा आठवीं बार जनवरी 2021 से दिसम्बर, 2022 तक चुना गया है।
प्रश्न 20.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्याख्या करें।
उत्तर:
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिन्हें महासभा तथा सुरक्षा परिषद् अलग-अलग स्वतन्त्र तौर पर चुनती है। जज 9 साल के लिए चुने जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों से सम्बन्धित सभी विषय इसके पास ले जाए जा सकते हैं।
प्रश्न 21.
अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) के कोई दो कार्य लिखें।
उत्तर:
- अन्तर्राष्टीय आण्विक ऊर्जा एजेन्सी परमाण उर्जा के शान्तिपर्ण उपयोग को बढावा देती है।
- अन्तर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेन्सी समय-समय पर परमाणु सुविधाओं की जांच करती है ताकि नागरिक संयन्त्रों का प्रयोग सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न किया जा सके।
प्रश्न 22.
एमनेस्टी इंटरनेशनल के कोई दो कार्य लिखें।
उत्तर:
- एमनेस्टी इंटरनेशनल सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व स्तर पर मानवाधिकारों से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करता है तथा उसे प्रकाशित करता है।
प्रश्न 23.
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के कोई दो कार्य लिखें।
उत्तर:
- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन विभिन्न देशों के मजदूरों के वेतन तथा काम करने का समय निश्चिय करता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन मज़दूरों में प्रचलित बेकारी को रोकने का प्रयास करता है।
प्रश्न 24.
सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यों के विशेषाधिकार को क्यों समाप्त नहीं किया जा सकता है ? कोई दो कारण दीजिए।
उत्तर:
(1) सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के विशेषाधिकार इसलिए समाप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पक्ष में इन देशों को विशेष महत्त्व दिया गया है।
(2) यदि स्थाई सदस्यों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाएं, तो हो सकता है कि इन शक्तिशाली देशों की रुचि संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे, तथा ये देश इस संगठन से बाहर आकर अपनी इच्छानुसार कार्य करना शुरू कर दें।
प्रश्न 25.
भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई दो तर्क दीजिए।
उत्तर:
(1) भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है।
(2) भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है।
प्रश्न 26.
भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता का विरोध करने वाले देशों के द्वारा दिए किन्हीं दो तर्कों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- आलोचक देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं।
- आलोचकों का कहना है, कि भारत पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को लेकर सुरक्षा परिषद् में अप्रभावी रहेगा।
प्रश्न 27.
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के नाम लिखिए।
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं-
- महासभा
- सुरक्षा परिषद्
- आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
- ट्रस्टीशिप कौंसिल
- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
- सचिवालय।
प्रश्न 28.
सुरक्षा परिषद् के कार्य लिखिए।
उत्तर:
- सुरक्षा परिषद् किसी ऐसे मामलों पर तुरन्त विचार कर सकती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के भंग होने का भय हो।
- सुरक्षा परिषद् आक्रामक कार्यवाहियों, विश्व शान्ति के लिए खतरे की सम्भावनाओं और शान्ति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकती है।

प्रश्न 29.
भारत ने विश्व शान्ति की स्थापना में क्या भूमिका अदा की है ?
उत्तर:
भारत ने विश्व शान्ति की स्थापना में बहुत-ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत उत्तर कोरिया के विरुद्ध भेजी गई सेनाओं में भारत ने भी अपनी सेना भेजी थी। सन् 1956 में मिस्त्र में स्वेज़ नहर के संकट को हल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर कांगों में अपनी सेनाएं भेजी तथा 1976 में अरब-इज़रायल विवाद को सुलझाने में अपना योगदान दिया।
प्रश्न 30.
विश्व के किन्हीं दो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
- संयुक्त राष्ट्र संघ-संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्तूबर, 1945, को विश्व में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी।
- विश्व व्यापार संगठन-विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों के विषय में नियम बनाने के लिए की गई थी।
प्रश्न 31.
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ लिखें।
उत्तर:
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ सम्प्रभु राज्यों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए संगठनों से लिया जाता है। टुंकिन के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों का ऐसा समूह है, जिसकी स्थापना सन्धि के आधार पर होती है तथा जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है।”
प्रश्न 32.
संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना की कोई दो व्यवस्थाएं बताएं।
उत्तर:
- भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषका से बचाना।
- मानवाधिकारों, मनुष्य के गौरव और उसके महत्त्व, पुरुषों एवं महिलाओं एवं छोटे और बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों पर विश्वास का अनुमोदन करना।
प्रश्न 33.
विश्व व्यापार संगठन कब बना?
उत्तर:
विश्व व्यापार संगठन सन् 1995 में बना।
प्रश्न 34.
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के पांच स्थाई सदस्य देशों के नाम लिखें।
उत्तर:
- अमेरिका
- इंग्लैण्ड
- फ्रांस
- रूस
- चीन।
प्रश्न 35.
“विश्व व्यापार संगठन” (W.T.0.) क्या है ?
उत्तर:
विश्व व्यापार संगठन का निर्माण 1 जनवरी, 1995 को हुआ था। यह संगठन विश्व व्यापार को नियमित और नियन्त्रित करने के लिए उत्तरदायी है। यह संगठन सभी सदस्य राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के व्यापार करने की व्यवस्था करता है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
1. निम्न में से किसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है ?
(A) सार्क
(B) आसियान
(C) संयुक्त राष्ट्र संघ
(D) यूरोपीयन संघ।
उत्तर:
(C) संयुक्त राष्ट्र संघ।
2. निम्न में से कौन-सा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है ?
(A) यूरोपीयन संघ
(B) आसियान
(C) सार्क
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
3. निम्न में से कौन-सा गैर सरकारी संगठन है ?
(A) अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सोसाइटी
(B) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(C) ह्यमन राइट्स वॉच
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं ?
(A) एन्टोनियो गुटेरस
(B) बुतरस घाली
(C) कोफी अन्नान
(D) सी० घनपाला।
उत्तर:
(A) एन्टोनियो गुटेरस।
5. निम्न में से कौन-सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है ?
(A) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
(B) विश्व स्वास्थ्य संगठन
(C) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
6. संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं
(A) 6
(B) 5
(C) 4
(D) 13
उत्तर:
(A) 6

7. संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दिक प्रस्ताव (Millennium Declaration) पर कब हस्ताक्षर किये गए ?
(A) सितम्बर, 1995
(B) जून, 1999
(C) सितम्बर, 2000
(D) मार्च, 2001
उत्तर:
(C) सितम्बर, 2000
8. संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ‘शान्ति निर्माण आयोग’ की स्थापना कब की गई ?
(A) दिसम्बर, 2005
(B) मार्च, 2003
(C) जून, 2002
(D) अगस्त, 2000
उत्तर:
(A) दिसम्बर, 2005
9. विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.0.) का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ?
(A) जेनेवा
(B) काठमाण्डू
(C) पेरिस
(D) लंदन।
उत्तर:
(A) जेनेवा।
10. संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना हुई ?
(A) वर्ष, 1951 में
(B) वर्ष, 1955 में
(C) वर्ष, 1941 में
(D) वर्ष, 1945 में।
उत्तर:
(D) वर्ष, 1945 में
11. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
(A) 395
(B) 111
(C) 174
(D) 152
उत्तर:
(B) 111
12. निम्न में से कौन-सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारम्भिक सदस्य है ?
(A) पाकिस्तान
(B) बंग्लादेश
(C) भारत
(D) नेपाल।
उत्तर:
(C) भारत।
13. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है
(A) लंदन में
(B) न्यूयार्क में
(C) नई दिल्ली में
(D) हेग में।
उत्तर:
(B) न्यूयार्क में।
14. प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे ?
(A) 47
(B) 46
(C) 51
(D) 55
उत्तर:
(C) 51
15. वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है
(A) 197
(B) 196
(C) 193
(D) 195
उत्तर:
(C) 193
16. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल होता है
(A) 2 वर्ष
(B) 4 वर्ष
(C) 5 वर्ष
(D) 6 वर्ष।
उत्तर:
(C) 5 वर्ष।
17. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है
(A) न्यूयार्क में
(B) बीजिंग में
(C) हेग में
(D) दिल्ली में।
उत्तर:
(C) हेग में।
18. ‘संयुक्त राष्ट्र बाल आपात्कालीन कोष’ (UNICEF) का मुख्यालय स्थित है :
(A) पेरिस में
(B) रोम में
(C) जेनेवा में
(D) न्यूयार्क में।
उत्तर:
(D) न्यूयार्क में।
19. वह पहला कौन-सा भारतीय था, जो महासभा का अध्यक्ष बना ?
(A) जवाहर लाल नेहरू
(B) सी० राजगोपालाचार्य
(C) एस० राधाकृष्णन
(D) विजयलक्ष्मी पण्डित।
उत्तर:
(D) विजयलक्ष्मी पण्डित।
20. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के कितने देश स्थायी सदस्य हैं ?
(A) 5
(B) 10
(C) 15
(D) 27
उत्तर:
(A) 5
21. संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का मुख्यालय कहां पर स्थित है ?
(A) बीजिंग में
(B) नई दिल्ली में
(C) हेग में
(D) न्यूयार्क में।
उत्तर:
(D) न्यूयार्क में।
22. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ?
(A) 108
(B) 99
(C) 111
(D) 102
उत्तरं:
(A) 108
23. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है ?
(A) न्यूयार्क में
(B) हेग में
(C) नई दिल्ली में
(D) ढाका में।
उत्तर:
(B) हेग में।
24. ‘यूनेस्को’ (UNESCO) का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ?
(A) नई दिल्ली
(B) पेरिस
(C) कराची
(D) लंदन।
उत्तर:
(B) पेरिस।
25. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना कब हुई ?
(A) 1 जनवरी, 1995 को
(B) 4 दिसम्बर, 1995 को
(C) 8 जनवरी, 1995 को
(D) 3 सितम्बर, 2000 को।
उत्तर:
(A) 1 जनवरी, 1995 को।
26. विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) अस्तित्व में कब आया ?
(A) 1 जनवरी, 1995 को
(B) 1 फरवरी, 1995 को
(C) 1 दिसम्बर, 1994 को
(D) 1 दिसम्बर, 1995 को।
उत्तर:
(A) 1 जनवरी, 1995 को।
27. निम्न एक भारतीय सन् 1982 में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गये थे ?
(A) डॉ० नगेंद्र सिंह
(B) डॉ० राधाकृष्णन
(C) एच० एम० बेग
(D) ए० एन० रे।
उत्तर:
(A) डॉ० नगेंद्र सिंह।
28. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मुख्यालय स्थित है :
(A) जेनेवा में
(B) न्यूयार्क में
(C) वाशिंगटन में
(D) पेरिस में।
उत्तर:
(D) जेनेवा में।
रिक्त स्थान भरें
(1) प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ……………….. को मनाया जाता है।
उत्तर:
24 अक्तूबर,
(2) संयुक्त राष्ट्र संघ में ……………….. मूल संस्थापक सदस्य हैं।
उत्तर:
51
(3) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ……………… 1945 को हुई।
उत्तर:
24, अक्तूबर
(4) भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का …………. देश है।
उत्तर:
संस्थापक
(5) संयुक्त राष्ट्र संघ के ………….. अंग हैं।
उत्तर:
6

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य …………….. की स्थापना करना है।
उत्तर:
विश्व शांति
(7) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल …………….. अनुच्छेद है।
उत्तर:
111
(8) संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या …… है।
उत्तर:
5
(9) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य …………. है।
उत्तर:
विश्व शांति
(10) सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या …………… है।
उत्तर:
5
एक शब्द/वाक्य में उत्तर दें
प्रश्न 1.
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं।
प्रश्न 2.
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयार्क में स्थित है।
प्रश्न 3.
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके कुल कितने सदस्य थे ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके कुल 51 सदस्य थे।
प्रश्न 4.
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है ?
उत्तर:
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
प्रश्न 5.
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है ?
उत्तर:
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है।
प्रश्न 6.
कौन-सी भारतीय नागरिक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी ?
उत्तर:
विजयलक्ष्मी पण्डित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी।