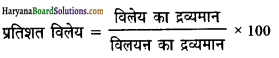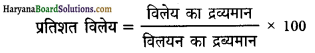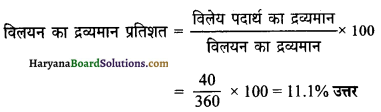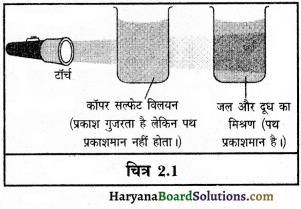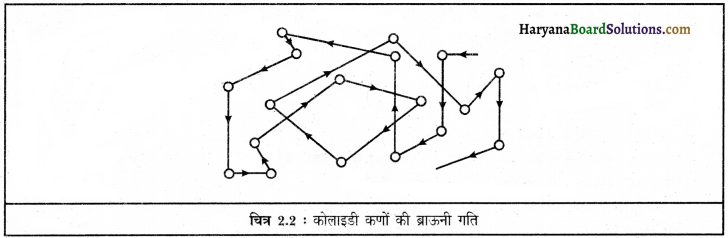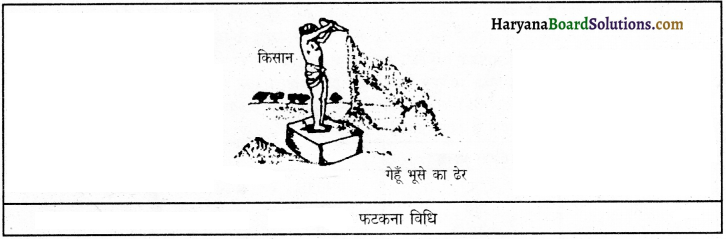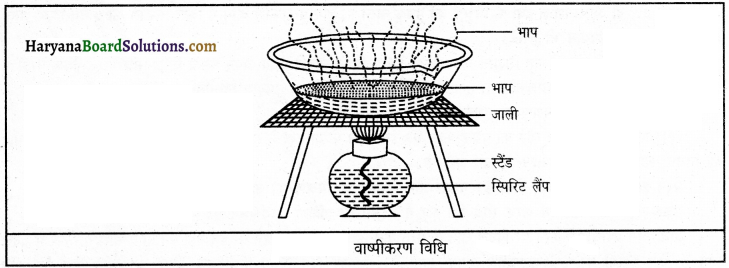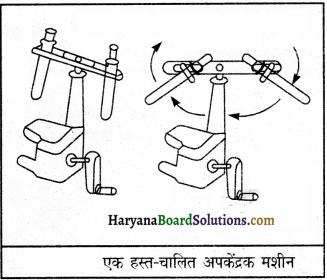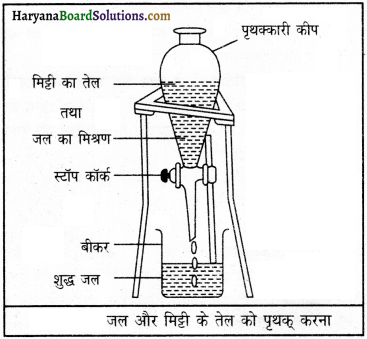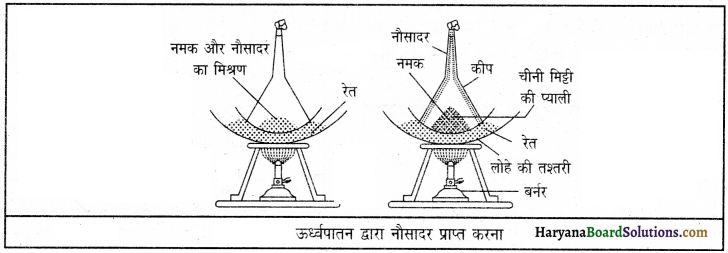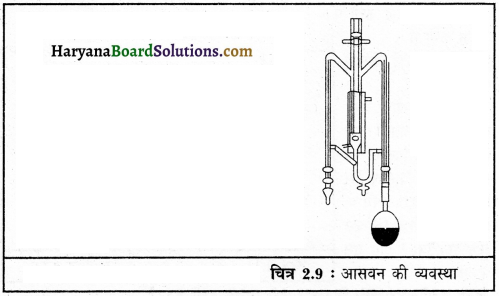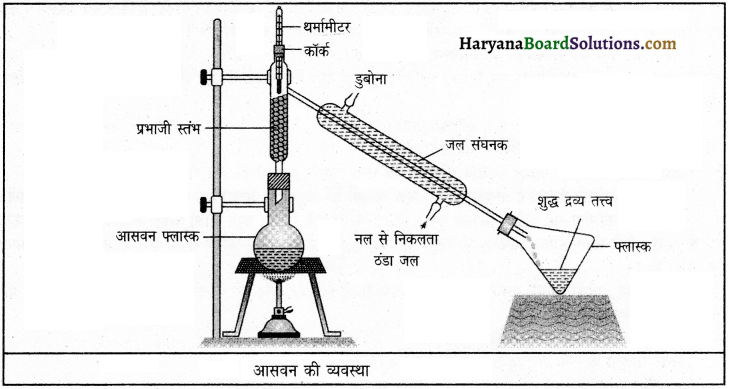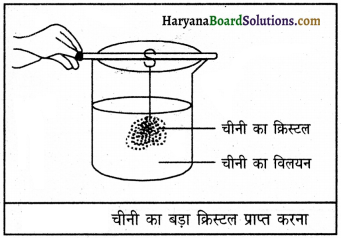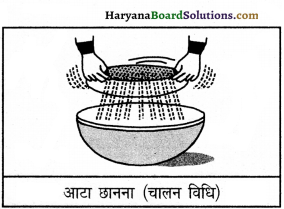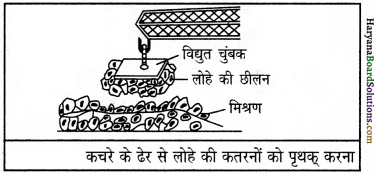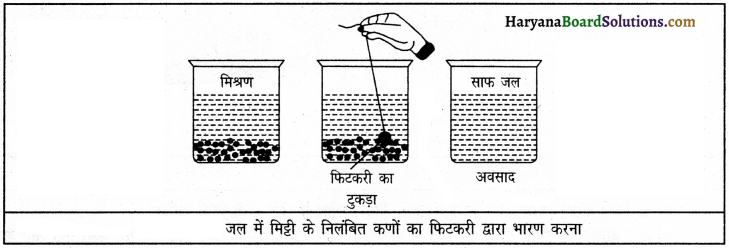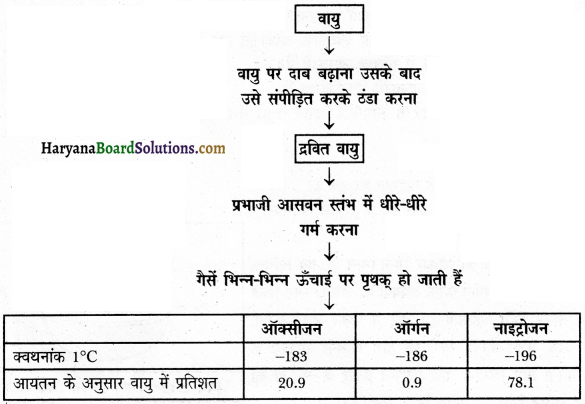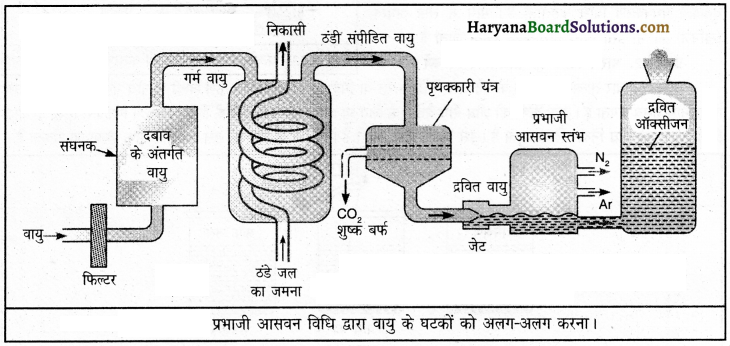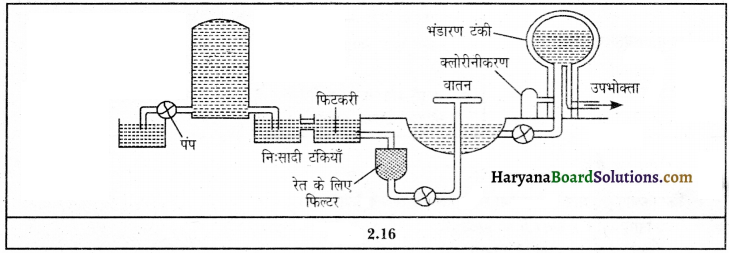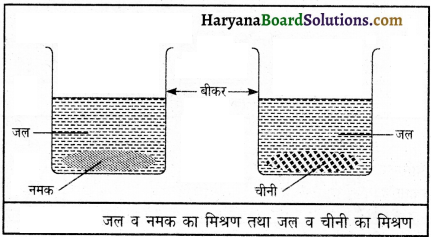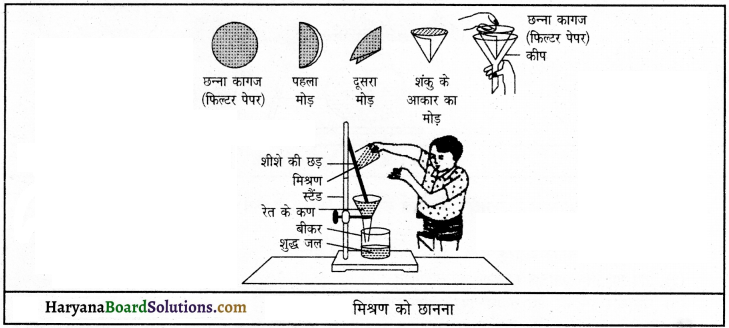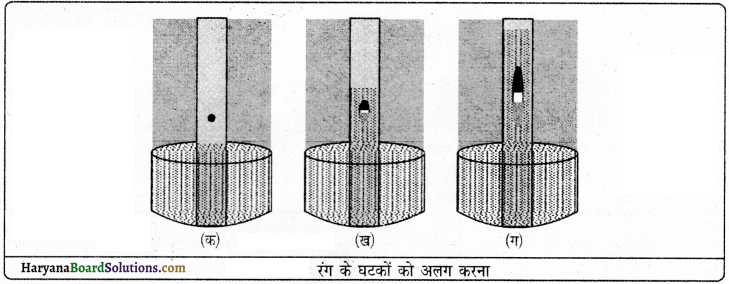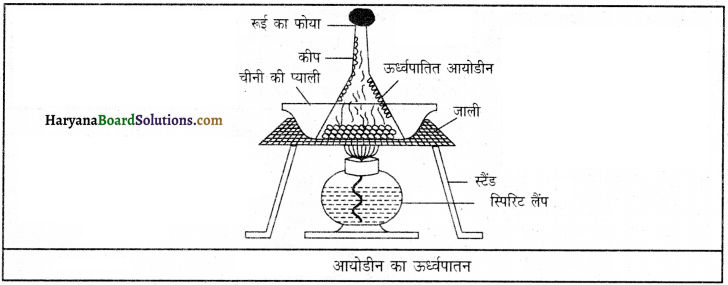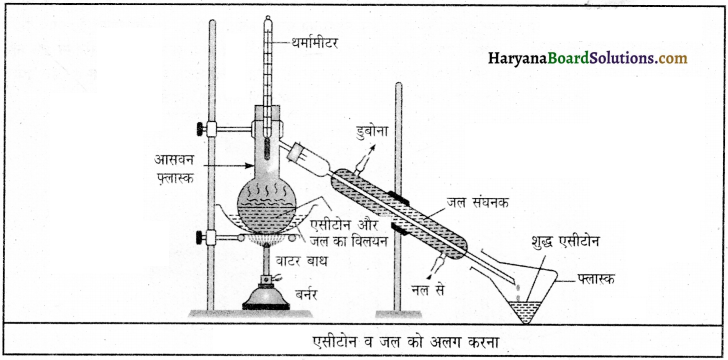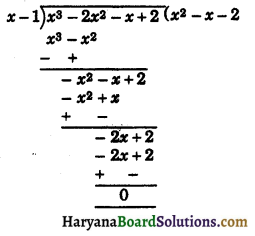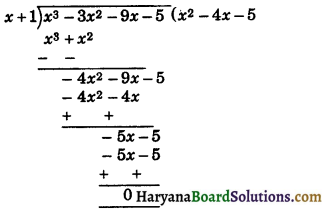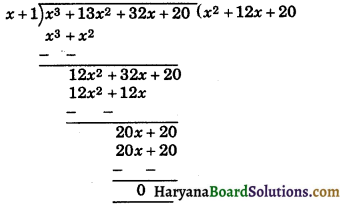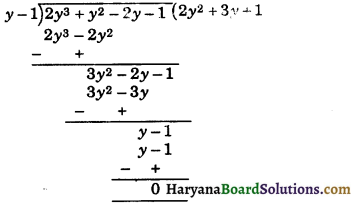Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका Important Questions and Answers.
Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 5 विधायिका
अति लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
न्यायपालिका किसे कहते हैं?
उत्तर:
न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्त्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना तथा अपराधियों को दण्ड देना है।
प्रश्न 2.
न्यायपालिका का महत्त्व बताइए।
उत्तर:
लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, “किसी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसके न्याय प्रबन्ध से बढ़िया कोई अन्य कसौटी नहीं।”
प्रश्न 3.
न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने के उपाय बताएँ।
उत्तर:
- न्यायाधीशों का अच्छा वेतन।
- न्यायाधीशों का लम्बा तथा निश्चित कार्यकाल।
प्रश्न 4.
न्यायाधीशों को अधिक वेतन देने के पक्ष में दो तर्क दीजिए।
उत्तर:
- न्यायाधीशों को अधिक वेतन देने से वे रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचे रह सकते हैं।
- वे निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय देने में सक्षम बन सकते हैं।

प्रश्न 5.
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है?
उत्तर:
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका विधानमण्डल, कार्यपालिका तथा किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह के दबाव अथवा प्रभाव से पूरी तरह स्वतन्त्र हो।
प्रश्न 6.
संसार के विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं तथा उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है?
उत्तर:
संसार के विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रायः तीन तरीके अपनाए जाते हैं
- जनता द्वारा चुनाव,
- विधानमण्डल द्वारा चुनाव,
- कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति।
इन तीनों तरीकों में से कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति ही अन्य दोनों तरीकों से अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें न्यायाधीशों पर दबाव की सम्भावना कम-से-कम होती है।
प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कुल कितना वेतन मिलता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,50,000 मासिक वेतन मिलता है।
प्रश्न 8.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए कोई दो योग्यताएँ लिखिए।
उत्तर:
- वह भारत का नागरिक हो।
- वह कम-से-कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अथवा कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो।
प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और किसकी सलाह से करता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों, जिन्हें वह उचित समझता है, की सलाह से करता है। .
प्रश्न 10.
सर्वोच्च न्यायालय को किन दो मामलों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
उत्तर:
- जब केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए।
- मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में।
प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय को किन दो मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
उत्तर:
- संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में।
- उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड की सजा दी हो।
प्रश्न 12.
सर्वोच्च न्यायालय के दो कार्य बताएँ।
उत्तर:
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना।
प्रश्न 13.
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन-कौन-से लेख जारी करता है?
उत्तर:
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख,
- परमादेश लेख,
- प्रतिषेध लेख,
- उत्प्रेषण लेख,
- अधिकार-पृच्छा लेख।
प्रश्न 14.
किन्हीं ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जिसका एक ही (साझा) उच्च न्यायालय है? वह कहाँ पर स्थित है?
उत्तर:
हरियाणा तथा पंजाब का एक ही साझा उच्च न्यायालय है जो चण्डीगढ़ में स्थित है।
प्रश्न 2.
न्यायपालिका का महत्त्व बताइए।
उत्तर:
लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, “किसी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसके न्याय प्रबन्ध से बढ़िया कोई अन्य कसौटी नहीं।
प्रश्न 3.
न्यायपालिका को स्वतन्त्र रखने के उपाय बताएँ।
उत्तर:
- न्यायाधीशों का अच्छा वेतन।
- न्यायाधीशों का लम्बा तथा निश्चित कार्यकाल।
प्रश्न 4.
न्यायाधीशों को अधिक वेतन देने के पक्ष में दो तर्क दीजिए।
उत्तर:
- न्यायाधीशों को अधिक वेतन देने से वे रिश्वत और भ्रष्टाचार से बचे रह सकते हैं।
- वे निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय देने में सक्षम बन सकते हैं।

प्रश्न 5.
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है?
उत्तर:
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका विधानमण्डल, कार्यपालिका तथा किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह के दबाव अथवा प्रभाव से पूरी तरह स्वतन्त्र हो।
प्रश्न 6.
संसार के विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन-कौन-से तरीके अपनाए जाते हैं तथा उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है?
उत्तर:
संसार के विभिन्न देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रायः तीन तरीके अपनाए जाते हैं-
- जनता द्वारा चुनाव,
- विधानमण्डल द्वारा चुनाव,
- कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति।
इन तीनों तरीकों में से कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति ही अन्य दोनों तरीकों से अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें न्यायाधीशों पर दबाव की सम्भावना कम-से-कम होती है।
प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कुल कितना वेतन मिलता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹2,50,000 मासिक वेतन मिलता है।
प्रश्न 8.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए कोई दो योग्यताएँ लिखिए।
उत्तर:
- वह भारत का नागरिक हो।
- वह कम-से-कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अथवा कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुका हो।
प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और किसकी सलाह से करता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों, जिन्हें वह उचित समझता है, की सलाह से करता है। .
प्रश्न 10.
सर्वोच्च न्यायालय को किन दो मामलों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
उत्तर:
- जब केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए।
- मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में।
प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय को किन दो मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
उत्तर:
- संविधान की व्याख्या के सम्बन्ध में।
- उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड की सजा दी हो।
प्रश्न 12.
सर्वोच्च न्यायालय के दो कार्य बताएँ।
उत्तर:
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना।
प्रश्न 13.
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन-कौन-से लेख जारी करता है?
उत्तर:
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख,
- परमादेश लेख,
- प्रतिषेध लेख,
- उत्प्रेषण लेख,
- अधिकार-पृच्छा लेख।
प्रश्न 14.
किन्हीं ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जिसका एक ही (साझा) उच्च न्यायालय है? वह कहाँ पर स्थित है?
उत्तर:
हरियाणा तथा पंजाब का एक ही साझा उच्च न्यायालय है जो चण्डीगढ़ में स्थित है।
प्रश्न 15.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है?
उत्तर:
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है।
प्रश्न 16.
किन्हीं दो मामलों में उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बताइए।
उत्तर:
- मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में।
- संविधान की व्याख्या सम्बन्धी।
प्रश्न 17.
चुनाव याचिकाएँ किस न्यायालय में पेश की जाती हैं?
उत्तर:
एम०एल०ए० (M.L.A.) तथा संसद सदस्य (M.P.) के चुनावों से सम्बन्धित चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालय में पेश की जाती हैं। राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित चुनाव याचिकाएँ केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश की जा सकती हैं।
प्रश्न 18.
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के दो तरीके बताइए।
उत्तर:
- न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती।
- न्यायाधीशों को संसद, महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हटा नहीं सकती।
प्रश्न 19.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता को किन दो तरीकों से सुनिश्चित किया गया है?
उत्तर:
- न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं और उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कटौती नहीं की जा सकती।
- दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के आरोपों की निष्पक्ष जाँच-पड़ताल होने पर संसद महाभियोग के अतिरिक्त न्यायाधीशों को अन्य किसी तरीके से नहीं हटा सकती।
प्रश्न 20.
क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश-प्राप्ति के बाद वकालत कर सकते हैं? क्या उन्हें जाँच आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश-प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें जाँच आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।
प्रश्न 21.
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता कैसे स्थापित की गई है?
उत्तर:
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है।
- उनको संसद महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से नहीं हटा सकती।
प्रश्न 22.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश-प्राप्ति के बाद कहाँ वकालत कर सकते हैं ?
उत्तर:
- सर्वोच्च न्यायालय में,
- दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में।
प्रश्न 23.
ऐसे दो मामले बताइए जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग किया हो?
उत्तर:
- ए०के० गोपालन केस, 1951,
- मेनका गाँधी केस, 1980।

प्रश्न 24.
न्यायिक सक्रियता के तीन साधन लिखें।
उत्तर:
न्यायिक सक्रियता के तीन साधन हैं
- न्यायिक पुनर्निरीक्षण,
- मौलिक अधिकारों की व्याख्या,
- संविधान की व्याख्या।
प्रश्न 25.
न्यायिक सक्रियता की आलोचना के तीन शीर्षक लिखें। अथवा न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तीन तर्क लिखिए।
उत्तर:
- संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध,
- न्यायपालिका के प्राथमिक कार्य में बाधा,
- प्रजातन्त्र के विरुद्ध।
प्रश्न 26.
न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में तीन तर्क लिखें।
उत्तर:
- सरकार को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक,
- मानवीय अधिकारों की रक्षा में सहायक,
- लोगों का समर्थन।
प्रश्न 27.
सार्वजनिक हित के लिए मुकद्दमेबाजी का क्या अर्थ है?
उत्तर:
जब कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह सार्वजनिक अथवा सामान्य हित के विषयों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो उसे सार्वजनिक हित की मुकद्दमेबाजी (P.I.L) कहा जाता है।
प्रश्न 28.
न्यायपालिका कितने प्रकार के लेख (Writ) जारी कर सकती है?
उत्तर:
न्यायपालिका निम्नलिखित पाँच प्रकार के लेख (Writ) जारी कर सकती है
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),
- परमादेश (Mandamus),
- प्रतिषेध (Prohibition),
- अधिकार पृच्छा (Quo-warranto),
- उत्प्रेषण (Certiorari)।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
न्यायपालिका का महत्त्व बताएँ।
उत्तर:
न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्त्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना तथा उन्हें तोड़ने वालों को दण्ड देना है। एक राज्य में विधानमण्डल तथा कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी तथा श्रेष्ठ क्यों न हो, परन्तु यदि न्याय-व्यवस्था दोषपूर्ण है अर्थात निष्पक्ष तथा स्वतंत्र नहीं है, तो नागरिकों का जीवन सुखी नहीं रह सकता। न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें सरकार के अत्याचार से बचाती है।
संघीय राज्यों में न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले झगड़ों का निपटारा करती है। लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने ठीक ही लिखा है, “किसी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की कुशलता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और वस्तु का नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित, शीघ्र तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था पर निर्भर करता है।”
प्रश्न 2.
न्यायपालिका के गठन पर प्रकाश डालो।
उत्तर:
न्यायपालिका का गठन भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न पाया जाता है। वास्तविकता में न्यायपालिका का गठन देश में पाई जाने वाली शासन-व्यवस्था पर निर्भर करता है। कई देशों में न्यायपालिका का एक निश्चित अवधि के लिए विधानपालिका द्वारा चुनाव किया जाता है। इसके विपरीत कुछ देशों में न्यायपालिका की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति का आधार न्यायाधीशों की योग्यताएँ होती हैं। न्यायाधीशों की अवधि भी भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होती है; जैसे भारत में न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं।
प्रश्न 3.
स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालय से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:
ब्राइस का यह कथन सत्य है कि किसी भी सरकार की श्रेष्ठता की सबसे अच्छी कसौटी न्यायपालिका की दक्षता है। न्यायपालिका की दक्षता उसकी निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता से है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका विधानमण्डल तथा कार्यपालिका से स्वतन्त्र हो। उस पर मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों का नियन्त्रण और प्रभाव न हो।
न्यायाधीश पक्षपात तथा बाहरी दबाव के आधार पर निर्णय न करें। न्यायाधीशों के निर्णयों पर किसी प्रकार का प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब न्यायाधीश पूर्णरूप से स्वतन्त्र हों। वे बिना किसी भय, लालच . तथा पक्षपात के पूर्ण न्याय करने वाले हों। न्यायाधीश योग्य, ईमानदार, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र हों। न्याय में देरी न हो। न्याय में देरी का अभिप्राय है-न्याय से इन्कार करना।।
प्रश्न 4.
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में सहायक चार तत्त्वों का वर्णन करें।
उत्तर:
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता में निम्नलिखित चार तत्त्व सहायक हैं
1. पद की अवधि-न्यायाधीशों को प्रलोभन तथा पक्षपात से दूर रखने के लिए न्यायाधीशों का कार्यकाल लम्बा रखा जाए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं।
2. पद से हटना-न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से न हटाया जा सके। पूरी छानबीन के पश्चात् ही एक विशेष विधि द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए।
3. अच्छा वेतन-न्यायाधीशों को अच्छा वेतन मिलना चाहिए, जिससे वे अपने समकक्ष दूसरे अधिकारियों की तरह आर्थिक स्तर स्थापित कर सकें।
4. योग्यता के आधार पर नियुक्ति-न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उनके ज्ञान, बुद्धि तथा योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए।
प्रश्न 5.
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:
किसी देश में कैसी भी शासन व्यवस्था की स्थापना क्यों न की गई हो, प्रत्येक सरकार के तीन. कार्य होते हैं; जैसे कानून बनाना, कानूनों को लागू करना तथा न्याय करना। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। यदि सरकार की तीनों शक्तियों को अलग-अलग रखा जाए तो इस सिद्धान्त को शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक मोण्टेस्क्यू का हना है कि सरकार की तीनों नहीं, दो शक्तियाँ भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिएँ। व्यक्तियों के अधिकार और स्वतन्त्रता की रक्षा तथा सरकार को निरंकुश होने से इस सिद्धान्त द्वारा ही रोका जा सकता है।

प्रश्न 6.
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की आलोचना के चार आधार बताएँ।
उत्तर:
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की आलोचना के आधार इस प्रकार हैं
- सरकार एक इकाई है तथा शरीर के अंगों के अनुसार कार्य करती है, अतः शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण सम्भव नहीं है,
- यह सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि शासन के सभी अंग एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं,
- शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण इसलिए भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सरकार के तीनों अंग समान नहीं हैं,
- मोण्टेस्क्यू का यह कथन उचित नहीं है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा अधिकार के लिए शक्तियों का पृथक्करण अनिवार्य है।
प्रश्न 7.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है?
उत्तर:
न्यायालय का यह वह अधिकार है जिसके प्रयोग से वह संसद अथवा राज्य विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता के बारे में निर्णय करता है और यदि वे संविधान के उल्लंघन में होते हैं तो उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द करने का अधिकार रखता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने ‘प्रिवी पर्स’ (Privy Purses) तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण (Nationalization of Banks) के आदेशों को इसी शक्ति के आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया था।
प्रश्न 8.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण के किन्हीं दो गुणों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
न्यायिक पुनर्निरीक्षण के गुण इस प्रकार हैं-
(1) भारत का संविधान लिखित है। लिखित संविधान की भाषा अथवा शब्दावली कहीं-कहीं अस्पष्ट तथा उलझी हुई हो सकती है। उसकी व्याख्या तथा स्पष्टीकरण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। संघीय शासन-प्रणाली में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। उनमें उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार महत्त्वपूर्ण है,
(2) नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिए भी न्यायालयों का यह अधिकार आवश्यक है, परन्तु यह बात भी ठीक है कि ये अधिकार असीमित नहीं हैं और राज्य की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उन पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध उचित है अथवा अनुचित, इसकी जाँच भी न्यायालय ही कर सकते हैं।
प्रश्न 9.
न्यायपालिका तथा विधायिका के सम्बन्धों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
उत्तर:
न्यायपालिका तथा विधायिका के सम्बन्ध इस प्रकार हैं-
(1) विश्व के कई देशों में न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, यदि वे संविधान के उल्लंघन में बनाए गए हैं। भारत तथा अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है,
(2) कई राज्यों में विधायिका न्यायपालिका के कई कार्यों का निष्पादन करती है। इंग्लैण्ड में संसद का उच्च सदन (हाउस ऑफ लॉर्ड्स) सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अमेरिका में सीनेट निचले सदन (प्रतिनिधि सदन) द्वारा दोषी बनाए गए कार्यपालिका के कर्मचारियों की जाँच की सुनवाई करती है,
(3) कई राज्यों (भारत) में विधायिका को न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) का प्रस्ताव पास करने का भी अधिकार है।
प्रश्न 10.
न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है?
उत्तर:
वर्तमान प्रजातन्त्रीय राज्यों में नागरिकों के विकास के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकार तथा स्वतन्त्रताएँ प्रदान की जाती हैं। न्यायपालिका नागरिकों के इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा करती है। भारतवर्ष में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी राज्यों के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है।
ये न्यायालय लेख (Writs) जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके साथ-ही-साथ यदि विधानपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जोकि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो ये न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की रक्षा करके विकास के अवसर प्रदान करती है।
प्रश्न 11.
न्यायपालिका संघीय ढाँचे के संरक्षक के रूप में कैसे कार्य करती है?
उत्तर:
जिस देश में संघीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था की गई है वहाँ न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। ऐसा शासन-प्रणाली में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसके द्वारा ही संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारों व कार्य-क्षेत्र को निश्चित किया जाता है। जब कभी केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो न्यायालय ही संविधान की सही व्याख्या कर उसका निर्णय करता है।
यदि संघीय अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई ऐसा कानून पास किया जाता है, जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका को उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द करने का अधिकार दिया जाता है। भारत तथा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
प्रश्न 12.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएँ क्या हैं?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यताएँ दी गई हैं-
- वह भारत का नागरिक हो,
- वह कम-से-कम पाँच वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। अथवा वह कम-से-कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रह चुका हो,
- वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधि-विशेषज्ञ हो।
प्रश्न 13.
उच्चतम न्यायालय का संगठन क्या है? इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर:
उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से सलाह करता है जिन्हें वह उचित समझता है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है।

प्रश्न 14.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों पर संक्षिप्त लेख लिखें। .
उत्तर:
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,80,000 मासिक वेतन मिलता है जबकि अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,50,000 मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त बिना किराए के मकान व अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। न्यायाधीशों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है जिस पर संसद की स्वीकृति मात्र औपचारिकता ही होती है। संसद न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन व भत्तों में कटौती नही कर सकती, हाँ, बढ़ा अवश्य सकती है। केवल वित्तीय संकट में उनके वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है।
प्रश्न 15.
सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करता है?
उत्तर:
यदि सरकार के किसी कार्य से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उस कार्य को अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है कि जिससे मौलिक अधिकार कम होते हो अथवा उनका हनन होता हो तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, मेनका गाँधी मामला इत्यादि में मौलिक अधिकारों की रक्षा की है।
प्रश्न 16.
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
उत्तर:
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए पहले न्यायाधीश का दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता का आरोप एक निष्पक्ष जाँच-पड़ताल द्वारा सिद्ध हो । उसके बाद संसद के दोनों सदन अलग-अलग रूप से सदन की कुल संख्या के बहुमत अथवा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रस्ताव को स्वीकृति देकर न्यायाधीश को पद से हटा देता है।
प्रश्न 17.
उच्चतम न्यायालय की संविधान के संरक्षक की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय को संविधान की व्याख्या तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका तथा विधायिका के उन सभी कार्यों व कानूनों को अवैध घोषित करता है जो संविधान का उल्लंघन करते हों। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधनों को भी अवैध घोषित किया है और अनेक मामलों में कहा है, “संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूलभूत ढाँचा विकृत होता हो अथवा नष्ट होता हो।”
प्रश्न 18.
न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायपालिका के उस अधिकार से है, जिसके अन्तर्गत न्यायपालिका संविधान के आधार पर कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के उन कार्यों व कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो कि न्यायालय के विचार में संविधान अथवा संविधान में निहित व्यवस्था का उल्लंघन करते हों। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को न्यायिक पनरावलोकन का अधिकार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से न्यायपालिका न्यायिक पनरावलोकन के अधिकार के अन्तर्गत संघीय व राज्य सरकारों के ऐसे कानूनों को भी अवैध घोषित करती है जिनमें इन सरकारों ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य संघात्मक व्यवस्था तथा संवैधानिक व्यवस्था व मूल्यों की रक्षा करना है।
प्रश्न 19.
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।
उत्तर:
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,50,000 मासिक वेतन मिलता है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त न्यायाधीशों को अनेक भत्ते व सुविधाएँ भी दी जाती हैं। न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। संसद न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन व भत्तों में कमी नहीं कर सकती, हाँ, बढ़ा अवश्य सकती है। केवल वित्तीय संकट में ही उनके (न्यायाधीशों के) वेतन व भत्तों में कटौती कर सकती है।
प्रश्न 20.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन-सी योग्यताएँ होना आवश्यक है?
उत्तर:
भारतीय संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए दी गई योग्यताएँ निर्धारित करता है-
- वह भारत का नागरिक हो,
- वह भारत में कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो।
प्रश्न 21.
न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करती है?
उत्तर:
मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का अति महत्त्वपूर्ण कार्य है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था यह समझे कि सरकार ने उसके या किसी और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वह अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में अथवा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार के लेख; जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश इत्यादि जारी कर सकती है और किसी भी कार्य तथा कानून को अवैध घोषित कर सकती है।
प्रश्न 22.
संविधान किस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की स्थापना करता है ?
उत्तर:
संविधान दिए गए उपायों व प्रावधानों से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करता है-
- न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है,
- न्यायाधीशों की नियुक्ति लम्बी अवधि के लिए की जाती है,
- कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती,
- न्यायाधीशों को समय से पूर्व केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है,
- न्यायाधीशों को संविधान में अनेक उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
प्रश्न 23.
उच्च न्यायालय की प्रशासन संबंधी शक्तियों का वर्णन कीजिये।
उत्तर:
उच्च न्यायालय को न्याय संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त कुछ प्रशासन संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं
- उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी भी न्यायालय के कागजों को मँगवाकर उनकी जाँच-पड़ताल कर सकता है,
- उच्च न्यायालय किसी मुकद्दमे को एक न्यायालय से हटाकर निर्णय के लिए दूसरे न्यायालय में भेज सकता है,
- यदि किसी न्यायालय में ऐसा मुकद्दमा चल रहा हो जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न पैदा होता है, तो उच्च न्यायालय उस मुकद्दमे को अपने पास मँगवाकर निर्णय दे सकता है,
- उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के शैरिफ, क्लर्क, वकील तथा अन्य कर्मचारियों की फीस निश्चित करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, अवनति, उन्नति और छुट्टी के बारे में नियम बनाता है,
- उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों की कार्य-पद्धति, रिकॉर्ड, रजिस्टर बना सकता है तथा हिसाब-किताब देख सकताहै,
- उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की देख-रेख करने तथा उन पर निरीक्षण रखने का अधिकार प्राप्त है।
प्रश्न 24.
न्यायिक सक्रियता के कोई चार कारण लिखें।
उत्तर:
न्यायिक सक्रियता के मुख्य चार कारण निम्नलिखित हैं
1. सरकार व देश में फैला व्यापक भ्रष्टाचार-वर्तमान समय में कुछ ही ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। न्यायालय भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करने में लगा हुआ है।
2. संविधान के नियमों का उल्लंघन सरकार द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा जब भी संविधान के नियमों की अवहेलना होती है तब न्यायपालिका ही हस्तक्षेप करके नियमों की या संविधान की रक्षा करती है।
3. लालसा-राजनेता जब सत्ता का स्वाद चख लेते हैं तो उनमें सत्ता में बने रहने की लालसा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का सक्रिय होना स्वाभाविक है।
4. विधानमण्डलों में अनुशासनहीनता-विधानमण्डलों में अनुशासनहीनता राजनेताओं का दैनिक कार्य बन चुका है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए न्यायपालिका की सक्रियता के इलावा और कोई चारा नहीं है।

प्रश्न 25.
न्याय सक्रियता के चार साधनों का वर्णन करो।
उत्तर:
1. न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायिक सक्रियता का पहला एवं महत्त्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार की शक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास है।।
2. मौलिक अधिकारों की व्याख्या-न्यायिक सक्रियता का दूसरा साधन मौलिक अधिकारों की व्याख्या से सम्बन्धित है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
3. संविधान की व्याख्या संविधान एक पवित्र पुस्तक मात्र है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है कि संविधान के विरुद्ध बने कानूनों को गैर-कानूनी घोषित कर उसकी सुरक्षा करे।
4. कानून निर्माण-न्यायपालिका का कार्य कानून निर्माण करना नहीं है फिर भी कानून की नई व्याख्या कानून निर्माण का कार्य करती है। यह न्यायिक सक्रियता का स्पष्ट उदाहरण है।
प्रश्न 26.
सर्वोच्च न्यायालय के प्रांरभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार क्षेत्र में वे मुकद्दमें आते हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायलय में ले जाए जा सकते हैं और जिनका सम्बन्ध संघीय व्यवस्था से है। ये इस प्रकार के हैं।
- संघ सरकार तथा एक अथवा अधिक राज्यों के बीच झगड़े।
- ऐसे झगड़े जिनमें संघीय सरकार तथा कुछ राज्य एक तरफ हों और कुछ अन्य राज्य तरफ हों।
- राज्यों के आपसी झगड़े जिनका सम्बन्ध कानून अथवा संविधान की व्याख्या से हो।
प्रश्न 27.
न्यायिक क्रियाशीलता से क्या तात्पर्य है।
उत्तर:
न्यायिक सक्रियवाद का अर्थ यह है कि न्यायपालिका द्वारा उन कार्यों को करना जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो कार्य विधानपालिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं और वे न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं। न्यायपालिका अन्य सरकारी सदस्यों को कुछ कार्य करने के निर्देश देती है और उनका पालन करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियावाद का अभिप्राय न्यायपालिका द्वारा अपनी शक्तियों के क्षेत्र में क्रियाशील भूमिका निभाना नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर होकर ऐसे काम करना है जो सरकार के अन्य अंगों के निर्धारित अधिकार क्षेत्र में होते हैं।
निबंधात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
आधुनिक लोकतन्त्रीय राज्यों में न्यायपालिका के कार्यों तथा शक्तियों की व्याख्या करें।
उत्तर:
न्यायपालिका सरकार का तीसरा तथा महत्त्वपूर्ण अंग है। यद्यपि यह विभाग उतना चर्चित नहीं जितने अन्य दोनों विभाग, फिर भी इसका महत्त्व किसी भी प्रकार अन्य विभागों से कम नहीं है। न्यायपालिका ही लोगों के अधिकारों तथा उनकी स्वतन्त्रताओं की रक्षा करती है तथा उन्हें अधिकारियों की निरंकुशता से बचाती है।
1. गार्नर (Garmer) के अनुसार, “बिना न्याय विभाग के किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है।” 2. लॉर्ड ब्राईस (Lord Bryce) का कथन है, “सरकार की उत्तमता की कसौटी उसकी न्यायपालिका की दक्षता है।” जिस राज्य के लोगों को निष्पक्ष तथा तुरन्त न्याय नहीं मिलता, वहाँ लोग सुखी नहीं रह सकते। इसलिए एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति अनिवार्य है।
न्यायपालिका के कार्य (Functions of Judiciary)- न्यायालय का मुख्य कार्य लोगों में न्याय वितरित करना है। यद्यपि न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय करना है तथा सार्वजनिक कानूनों को व्यक्तिगत मामलों में लागू करना है, परन्तु न्याय करने के अतिरिक्त भी न्यायपालिका को बहुत-से कार्य करने पड़ते हैं। न्यायपालिका के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं
1. अपराधियों को दण्ड देना-न्यायपालिका का कार्य अपराधियों को दण्ड देना है जिससे दूसरे व्यक्ति अपराध न करें। जब कोई व्यक्ति राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे उपयुक्त दण्ड देता है।
2. विवादों का निर्णय करना-न्यायालय लोगों के आपसी दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी विवादों का फैसला करता है। यदि निम्न न्यायालयों के निर्णय से कोई पक्ष असन्तुष्ट रहे तो उसे उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दोनों पक्षों को मानना पड़ता है।
3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना-राज्य व्यक्ति को अपने विकास के लिए बहुत-से अधिकार प्रदान करता है। जिन देशों के संविधान लिखित होते हैं, वहाँ नागरिकों को संविधान द्वारा ही बहुत-से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नागरिकों के सभी अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। यदि न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न की जाए तो अधिकार अर्थहीन बन जाते हैं।
4. कानून को व्यक्तिगत मामलों में लागू करना राज्य अलग-अलग लोगों तथा वर्गों के लिए अलग-अलग कानून नहीं बनाता। कानून सभी के लिए समान रूप से बनाए जाते हैं। न्यायपालिका सार्वजनिक कानूनों को व्यक्तिगत मामलों में लागू करते हैं।
5. कानूनों की व्याख्या विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानून सामान्य होते हैं। इनकी विस्तार सहित व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य है। विभिन्न पक्ष अपने-अपने ढंग से कानून का अर्थ लगाते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय ही उसकी सही व्याख्या करता है। न्यायालय की व्याख्या अन्तिम होती है, जिसे सबको मानना पड़ता है।
6. नए कानूनों का निर्माण-जब न्यायालय के सामने कोई ऐसा विवाद आता है, जिसके सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है तो न्यायाधीश अपनी योग्यता व निष्पक्षता के आधार पर न्याय करते हैं। उनका यह निर्णय कानून बन जाता है। भविष्य में उसी के आधार पर न्याय किया जाता है। ऐसे कानूनों को न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून (Judge made Laws) कहा जाता है।
7. संविधान की रक्षा-न्यायालय देश के संविधान का संरक्षक होता है। यदि कार्यपालिका अथवा विधानपालिका द्वारा संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय उनके कार्यों को अवैध घोषित करके निरस्त कर सकता है। संविधान की रक्षा करना न्यायालय का ही कार्य है। वह केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संविधान विरोधी कार्यों को निरस्त कर देता है। इस प्रकार संविधान की सुरक्षा बनी रहती है।
8. परामर्श सम्बन्धी कार्य आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका राज्याध्यक्ष को कानूनी सलाह भी देता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से किसी भी मामले में कानूनी सलाह ले सकता है। न्यायालय के परामर्श को मानना अथवा न मानना राष्ट्रपति का कार्य है।
9. विविध कार्य-न्यायपालिका अन्य कई विविध कार्य भी करती है। आन्तरिक प्रबन्ध करना, अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, विविध प्रकार की आज्ञाएँ जारी करके अधिकारियों के किसी अनुचित कार्य को रोकना न्यायालय का कार्य है। नाबालिगों की सम्पत्ति के लिए ट्रस्टी नियुक्त करना, स्त्रियों तथा पागलों के लिए संरक्षक नियुक्त करना, व्यक्तियों की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना, दिवालियों की सम्पत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त करना भी न्यायालय के कार्य हैं। इनके अतिरिक्त विवाह तथा तलाक को मान्यता देना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना आदि भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस तरह न्यायपालिका का काम न्याय करना ही नहीं, अन्य और भी बहुत से कार्य करना है।
प्रश्न 2.
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का महत्त्व बताइए। न्यायपालिका को निष्पक्ष या स्वतन्त्र कैसे रखा जा सकता है ?
उत्तर:
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अभिप्राय है कि वह विधानमण्डल तथा कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त हो। उस पर मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों का प्रभाव न हो। न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण तथा किसी तरह के बाहरी दबाव में आकर न्याय न करें। न्यायाधीशों के निर्णयों पर किसी प्रकार का प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब न्यायाधीश पूर्णरूप से स्वतन्त्र हों। वे बिना किसी भय, लालच अथवा पक्षपात के पूर्ण न्याय करने वाले हों।
स्वतन्त्र न्यायपालिका का महत्त्व स्पष्ट है। देश के कानून चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, वास्तविक न्याय तब तक नहीं हो सकता, जब तक न्यायाधीश योग्य, ईमानदार, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न हों। यदि न्याय करने में देरी लगती है या भेदभाव रखा जाता है तो लोगों के जान व माल की रक्षा सम्भव नहीं। स्वतन्त्र न्यायपालिका ही जनता के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की संरक्षक है।
यदि न्याय रूपी दीपक बुझ जाता है तो कितना गहन अन्धकार होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। – प्रजातन्त्र की सफलता भी इस बात पर निर्भर है, इसलिए लॉर्ड ब्राइस का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि किसी भी सरकार की श्रेष्ठता की सबसे अच्छी कसौटी न्यायपालिका की दक्षता है। एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था संगठित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए
1. न्यायाधीशों की नियुक्ति-न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए न्यायाधीशों का उचित ढंग से नियुक्त किया जाना बहुत अनिवार्य है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति के निम्नलिखित तीन तरीके प्रचलित हैं
(1) जनता द्वारा चुनाव-जनता द्वारा चुनाव करने की प्रथा रूस तथा अमेरिका में निम्नतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में अपनाई जाती है, परन्तु यह पद्धति अत्यन्त दोषपूर्ण है। जनता यह नहीं जानती कि कौन व्यक्ति न्यायाधीश बनने के योग्य है। दूसरे, न्यायाधीश अपने मतदाताओं को खुश रखने का प्रयत्न करेंगे जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। तीसरे, इस विधि से केवल राजनीतिज्ञ ही न्यायाधीश बन सकेंगे जो किसी भी रूप में उचित नहीं है।
(2) विधानमण्डल द्वारा चुनाव-विधानमण्डल द्वारा चुनाव की पद्धति रूस तथा स्विट्ज़रलैण्ड के उच्च न्यायालयों के लिए अपनाई जाती है। यह विधि भी ठीक नहीं है, क्योंकि विधायक योग्य नहीं होते। विधानसभा में बहुमत दल का प्रभाव होता है, इससे न्यायाधीश भी दलबन्दी में फंसकर कार्य करेंगे। वे न्याय करने की जगह अपने निर्वाचकों को खुश करने के प्रयत्न में ही लगे रहेंगे।
(3) कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति सबसे अच्छी है। इसमें कार्यपालिका व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नियुक्ति करेगी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह कार्य राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है।
2. पद की अवधि-न्यायाधीशों को प्रलोभन तथा पक्षपात से दूर रखने के लिए उनका सेवाकाल भी लम्बा रखा जाना अनिवार्य है। यदि न्यायाधीशों का कार्यकाल थोड़ा होगा तो वे भविष्य के लिए रिश्वत लेने से भी नहीं हिचकेंगे, इसलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल लम्बा होना चाहिए जिससे वे अपने पद के दौरान अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। आज न्यायाधीश ‘सदाचार पर्यन्त पद’ (Good Behaviour Tenure) के सिद्धान्त पर एक लम्बे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।
3. न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि अयोग्य तथा दुराचारी व्यक्ति को न्याय के पद पर नहीं रहने देना चाहिए। यदि न्यायाधीश गलत काम करें तो उन्हें अपने पद से हटा देना चाहिए, परन्तु न्यायाधीशों का हटाया जाना इतना सरल तथा सुलभ न हो कि झूठा दोष लगाकर किसी भी न्यायाधीश को हटा दिया जाए। न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा विधानपालिका के दोषारोपण करने तथा उसकी जाँच-पड़ताल करने पर ही हटाया जाना चाहिए। भारत में संसद द्वारा महाभियोग सिद्ध होने पर ही राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकता है, अन्यथा नहीं।
4. न्यायाधीशों का अच्छा वेतन-उचित न्याय के लिए न्यायाधीशों को प्रलोभनों से मुक्त रखा जाए। इसलिए उन्हें इतना वेतन अवश्य दिया जाए, जिससे वे अपने समकक्ष दूसरे अधिकारियों की तरह आर्थिक स्तर स्थापित कर सकें। उनको वेतन समय पर मिले तथा वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ उनके कार्यकाल में कम न किए जाएँ। ऐसा होने पर ही न्यायाधीशों से निष्पक्ष तथा ईमानदार होकर न्याय करने की अपेक्षा की जा सकती है।
5. योग्यता के आधार पर नियुक्ति न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय उनके ज्ञान, बुद्धि तथा योग्यताएँ भी देखी जानी चाहिएँ। न्याय कार्य अन्य शासन कार्यों से भिन्न है। इसके लिए उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो कानून तथा न्याय सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान रखते हों। उन्हें देश के कानूनों तथा परम्पराओं का पर्याप्त ज्ञान हो।
6. सेवा निवृत्त होने पर वकालत की मनाही न्यायाधीशों के सम्मान तथा निष्पक्षता के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें वकालत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वर्तमान न्यायाधीश अपने पुराने साथियों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं।
7. विधानपालिका तथा कार्यपालिका से पृथक्कता-न्यायपालिका को विधानपालिका तथा कार्यपालिका से पृथक् रखा जाना चाहिए अन्यथा न्यायाधीश स्वतन्त्र रूप से न्याय नहीं कर सकेंगे। एक स्वतन्त्र न्यायालय जनता के अधिकारों व स्वतन्त्रता की रक्षा का दुर्ग है। भारत में न्यायपालिका को विधानपालिका तथा कार्यपालिका से स्वतन्त्र रखा गया है। न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं तथा विधानपालिका ही महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पास कर सकती है।
तभी न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं। निष्कर्ष-उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इन विधियों को अपनाने से न्यायपालिका को स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रखा जा सकता है। इन विधियों को अपनाए बिना न्यायपालिका का स्वतन्त्र रूप से कार्य करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न 3.
उच्चतम न्यायालय के संगठन एवं रचना का वर्णन करें।
उत्तर:
भारतीय संविधान एक एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) है। इसके संगठन, शक्तियाँ तथा कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं रचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारम्भ में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे।
1957 में संसद में एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी न्यायाधीशों की संख्या 7 से 10 कर दी गई। सन् 1960 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी, परन्तु दिसम्बर, 1977 में संसद ने एक कानून पास किया, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। अप्रैल, 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई।
21 फरवरी, 2008 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के निर्णयानुसार उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को 25 से 30 कर दी गई। जबकि संसद द्वारा (लोकसभा द्वारा 5 अगस्त एवं राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त) पारित सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 के उपरान्त 10 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गई।
इस प्रकार अब एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। वर्तमान में श्री शरद अरविंद बोबड़े सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने श्री रंजन गोगोई के 17 नवम्बर, 2019 को सेवानिवृत होने के बाद 18 नवम्बर, 2019 को 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार सम्भाला जो 23 अप्रैल, 2021 तक अपने पद पर रहेंगे।
न्यायाधीशों की नियुक्ति-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों व उच्च न्यायाधीशों, जिन्हें वह उचित समझता है, से सलाह करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त के पालन’ की परम्परा विकसित करने का प्रयास किया गया है।
हालाँकि दो बार इस परम्परा का राजनीतिक कारणों से उल्लंघन किया गया है। 1973 में श्री हेगड़े, श्री शैल व श्री ग्रोवर की वरिष्ठता की उपेक्षा करके श्री ए०एन० रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करता है। हालाँकि न्यायाधीशों की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
न्यायाधीशों की योग्यताएँ संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निश्चित की गई योग्यताएँ इस प्रकार हैं-
- वह भारत का नागरिक हो,
- वह किसी एक या दो अथवा दो से अधिक उच्च न्यायालयों का निरन्तर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो,
- वह कम-से-कम 10 वर्ष तक एक अथवा दो से अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत कर चुका हो,
- वह राष्ट्रपति के विचार में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Jurist) हो।
शपथ उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश अपना पद सम्भालने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के सम्मुख यह शपथ लेते हैं, “भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान् रहेंगे, उसमें सच्चा विश्वास रखेंगे, अपने कार्य को अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान एवं न्याय की भावना सहित और निर्भीक व निष्पक्ष, बिना प्रेम या बुरी इच्छा के साथ निष्ठा से निभाएँगे तथा भारतीय संविधान व कानून की पुष्टि करेंगे।”
वेतन-उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,50,000 मासिक वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते, अवकाश तथा निःशुल्क निवास स्थान भी मिलता है। किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात् संसद द्वारा उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती। सेवा से मुक्त होने के पश्चात् उन्हें पेन्शन (Pension) भी दी जाती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन केवल आर्थिक संकट की दशा में . ही कम किया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
कार्यकाल-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायापालिका की स्वतन्त्रता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया कि वह अपनी इच्छानुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सके। 65 वर्ष की आयु से पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है या उसकी मृत्यु से उसका पद रिक्त हो सकता है।
इसके अतिरिक्त उन्हें बुरे व्यवहार व अयोग्यता के आधार पर ही 65 वर्ष की आयु से पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की यह विधि महाभियोग के समान है। बुरे व्यवहार व अयोग्यता का यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग उनके कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एक ही अधिवेशन में संसद द्वारा न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुए बिना राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटा सकता।
उच्चतम न्यायालय का कार्य स्थान साधारणतया उच्चतम न्यायालय का कार्य स्थान नई दिल्ली निश्चित किया गया है, परन्तु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति व पूर्वाज्ञा द्वारा इसकी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी बुला सकता है। सेवा मुक्त होने के पश्चात् वकालत की मनाही-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, परन्तु उन्हें किसी आयोग के सदस्य, राज्यपाल, राजदूत आदि उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।
प्रश्न 4.
भारत के उच्चतम न्यायालय का संगठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करो। अथवा उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। अथवा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान संघात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना के साथ-साथ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना भी करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) शीर्ष पर है। भारतीय न्यायपालिका को संविधान-निर्माताओं ने स्वतन्त्र व निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रावधान संविधान में ही कर दिए हैं।
संविधान में न्यायपालिका की संविधान की संरक्षक, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक, लोकतन्त्र व जन-कल्याण में सहायक तन्त्र के रूप में भूमिका निर्धारित की गई है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनराविलोकन (Judicial Review) का अधिकार भी सौंपता है जिसके अन्तर्गत न्यायपालिका किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका उच्च विधायिका (Super Legislature) नहीं है। भारत में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का वर्णन निम्नलिखित है
उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अथवा शक्ति (Power of Jurisdiction of Supreme Court)-श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (Sh. Aladi Krishna SwamiAiyar) के अनुसार, “भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विश्व के किसी भी संघात्मक राज्य के उच्चतम न्यायालय से अधिक है। यहाँ तक कि यह अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भी अधिक शक्तिशाली है।” उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ इस प्रकार हैं-
- प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार,
- अपीलीय क्षेत्राधिकार,
- परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार,
- संविधान का व्याख्याकार,
- निर्णयों का पुनर्निरीक्षण,
- अभिलेख का न्यायालय,
- अन्य अधिकार,
- संविधान का संरक्षक।
1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्रधिकार निम्नलिखित हैं
(क) संघीय मामले इस अधिकार क्षेत्र में वे मुकद्दमे आते हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय के पास ले जाए जा सकते हैं और जिनका सम्बन्ध संघीय व्यवस्था से है। इन्हें किसी निम्न न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय का निम्नलिखित विषयों में एकमात्र प्रारम्भिक क्षेत्र है-
- संघ सरकार तथा एक अथवा अधिक राज्यों के मध्य झगड़े,
- ऐसे. झगड़े जिसमें संघ सरकार और कुछ राज्य एक ओर हों और कुछ राज्य दूसरी ओर हों,
- राज्यों के पारस्परिक झगड़े जिनका सम्बन्ध कानून एवं संविधान की व्याख्या से हो।
अपवाद उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित विषय किसी अन्य न्यायालय में पेश नहीं किए जा सकते, परन्तु निम्नलिखित प्रकार के विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते
(1) उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में केवल वही मुकद्दमे आते हैं जिनका सम्बन्ध कानूनी प्रश्न या तथ्य (Legal Question on Fact of Law) से हो अर्थात् राजनीतिक प्रकृति के विवाद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते,
(2) उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में वे मामले नहीं आते जिनका सम्बन्ध किसी ऐसी सन्धि, समझौते आदि से हो जो संविधान के लागू होने से पहले किए गए हों और जो अब तक निरन्तर जारी हों अथवा जिनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि उनके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे संविधान के.सातवें संशोधन के अनुसार भारत सरकार की देशी रियासतों के राजाओं से की हुई सन्धियाँ इस क्षेत्र में नहीं आतीं,
(3) उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में वे विवाद भी नहीं आते जिनका सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय नदियों (Inter-State Rivers), नदी घाटियों (River Valleys) तथा जल के वितरण आदि से हो,
(4) किसी नागरिक तथा किसी राज्य या भारत सरकार के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी झगड़े को सीधा उच्चतम न्यायालय में नहीं लाया जा सकता।
(ख) मौलिक अधिकारों का संरक्षक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना भी उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में आता है। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अधिकारों तथा संविधान का संरक्षक है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का सरकार तथा अन्य संस्था द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या प्रतिलेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिनके द्वारा यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये लेख हैं बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus), प्रतिषेध लेख (Writ of Prohibition), परमादेश लेख (Writ of Mandamus), उत्प्रेषण लेख (Writ of Certiorari) तथा अधिकार पृच्छा लेख (Writ of Quo-Warranto)।
(ग) राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी झगड़े-राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित सभी विवादों के निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं और इस प्रकार यह इसके प्रारम्भिक अधिकार के अन्तर्गत आता है।
(घ) संघीय लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को महाभियोग के द्वारा तभी हटाया जा सकता है, जबकि इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय सदस्यों पर लगे आरोपों की पुष्टि कर दे अर्थात् आयोग के सदस्यों के विरुद्ध लगे आरोपों की जाँच करने का एकमात्र अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार-अपीलीय क्षेत्राधिकार से अभिप्राय उन विवादों से है जो आरम्भ तो उच्च न्यायालयों या निम्न न्यायालयों में होते हैं, लेकिन निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
(क) संवैधानिक मामले-किसी मुकद्दमे में अपना निर्णय देते हुए यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि यह विवाद संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित है तो उसके विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देने से इन्कार कर दे तो उच्चतम न्यायालय स्वयं भी संविधान के अनुच्छेद 132 के अन्तर्गत अपने सम्मुख अपील करने की आज्ञा दे सकता है।
(ख) फौजदारी मुकद्दमे-संविधान के अनुच्छेद 134 के अधीन फौजदारी मुकद्दमों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालयों के सामने उस समय अपील की जा सकती है यदि-
(1) किसी अभियुक्त को निम्न अदालत ने छोड़ दिया था, परन्तु उच्च न्यायालय ने अपील में उसे मृत्यु-दण्ड दिया हो तो अभियुक्त उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है,
(2) यदि उच्च न्यायालय किसी फौजदारी मामले को निम्न न्यायालय से अपने पास मँगवाकर अभियोग की सुनवाई स्वयं करे और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दे,
(3) ऐसे फौजदारी मामलों की अपील भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है जिनके बारे में उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि अमुक मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन सुनवाई हेतु जा सकता है।
(ग) दीवानी अपीलें संविधान के अनुच्छेद 133 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को दीवानी अभियोगों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसी अपील उसके सामने उसी समय की जा सकती है, जब उच्च न्यायायल यह प्रमाण पत्र दे कि इस मुकद्दमे में सार्वजनिक महत्त्व या हित का कोई कानूनी प्रश्न उलझा हुआ है और उसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है।
संविधान के 30वें संविधान संशोधन द्वारा बीस हजार रुपए वाली शर्त समाप्त कर दी गई है। दूसरे शब्दों में बीस हजार से कम या अधिक का कोई मामला तभी अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में आएगा जब उसमें सामान्य हित का कोई कानूनी प्रश्न उलझा हुआ है।
1) विशेष अपीलें-संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अभियोग के विषय में निम्न न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसे यह अधिकार सैनिक न्यायालयों के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं है।
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार-संविधान के अनुच्छेद 143 द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मामले पर उच्चतम न्यायालय से कानूनी सलाह माँग सकता है। ऐसे मामले पर कम-से-कम पाँच न्यायाधीश बैठकर विचार करते हैं और बहुमत से निर्णय करके निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अभी तक उच्चतम न्यायालय के इस परामर्शदात्री कार्य का राष्ट्रपति द्वारा बराबर सम्मान किया गया है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से सलाह 1958 में केरल शिक्षा विधेयक के बारे में माँगी थी। अब तक अनेक बार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे चुका है।।
4. संविधान का व्याख्याका-संविधान की अन्तिम व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। इस अधिकार के अन्तर्गत न्यायालय को पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय संसद तथा राज्य विधान-मण्डलों द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
5. निर्णयों का पुनर्निरीक्षण-संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा किए गए निर्णयों को दृष्टान्त या मिसाल के रूप में न मानकर कानून की नई व्याख्या करने की शक्ति दी गई है।
6. अभिलेख का न्यायालय उच्चतम न्यायालय अभिलेख का न्यायालय भी है। उसके निर्णय तथा कार्रवाई को भविष्य में उदाहरणार्थ पेश करने के लिए लिपिबद्ध करके रखा जाता है।
7. अन्य अधिकार-उच्चतम न्यायालय को अन्य दूसरे कार्य करने का अधिकार भी है। इन कार्यों में
- उच्चतम न्यायालय उन लोगों को दण्ड दे सकता है जो इसका अपमान करें,
- उच्चतम न्यायालय के आदेश और निर्णय भारत के सभी असैनिक न्यायालय तथा पदाधिकारियों को मानने पड़ते हैं,
- भारत के सभी असैनिक न्यायालय इसके नियन्त्रण में हैं। यह किसी भी न्यायालय को कोई भी आदेश दे सकता है। अभियोगों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है। यह किसी भी तरह की सूचना मँगवा सकता है,
- वह अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करता है। उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की दूसरी शर्तों को निश्चित करता है,
- उच्चतम न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है,
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेता है,
- उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयों के फैसले, डिग्री, दण्ड, आज्ञा के विरुद्ध अपने आगे अपील करने की आज्ञा दे सकता है,
- कोई भी नागरिक या सरकारी कर्मचारी न्यायालय के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे दण्ड दिया जा सकता है।
8. संविधान का संरक्षक-उच्चतम न्यायालय को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति संविधान के संरक्षक के रूप में प्राप्त है। इसके अधीन उच्चतम न्यायालय कानूनों के साथ-साथ उन संविधान संशोधनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो उसके विचार में संविधान का उल्लंघन करते हों। अपने इस अधिकार के अन्तर्गत केशवानन्द भारती मामले सन् 1973 में उच्चतम न्यायालय ने संसद के संशोधन सम्बन्धी अधिकार को सीमित करते हुए कहा था, “संसद ऐसा कोई कानून या संविधान में संशोधन नहीं कर सकती कि जिससे संविधान का मूलभूत ढाँचा विकृत अथवा नष्ट होता हो।”
निष्कर्ष-उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ तथा कार्य उसे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अति महत्त्वपूर्ण बना देते हैं। उच्चतम न्यायालय संघात्मक व्यवस्था के रक्षक, संविधान के रक्षक, संविधान के व्याख्याकार, मौलिक अधिकारों के रक्षक की भूमिका निभाने के साथ-साथ लोकतन्त्र व जनकल्याण के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाता है।
च्चतम न्यायालय दलित व गरीब लोगों के लिए न्याय का अन्तिम शरणगाह है। उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद (Public Interest Litigation) के द्वारा अपने अधिकारों व शक्तियों में असीमित वृद्धि कर ली है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में कहा है, “न्यायपालिका कानूनों व संविधान की व्याख्याकार मात्र नहीं है, बल्कि न्याय की अन्तिम शरणस्थली है।” उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा संसद व कार्यपालिका की शक्ति को सीमित करके लोकतन्त्र की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्रश्न 5.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यताओं, कार्यकाल तथा वेतन का वर्णन करो। अथवा राज्य के उच्च न्यायालय की रचना तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन करो।
उत्तर:
परिचय (Introduction) भारत में एकल न्याय-व्यवस्था है, सबसे ऊँचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 231 में यह भी कहा गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों और केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। सन् 1966 के पंजाब पुनर्गठन कानून के द्वारा संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्यों और चण्डीगढ़ के केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया, जो चण्डीगढ़ में है। राज्यों के ये उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्याय-व्यवस्था का अंग होते हुए भी अपने आप में स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं।
उनके ऊपर अपने राज्यों के विधानमण्डल या कार्यपालिका का कोई नियन्त्रण नहीं है। मार्च, 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के अलग से उच्च न्यायालय अस्तित्व में आने पर कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से बढ़कर 24 हुई थी जो 1 जनवरी, 2019 को आन्ध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती में आन्ध्रप्रदेश राज्य का अलग उच्च न्यायालय अस्तित्व में आने के बाद देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 हो गई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आन्ध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना दो अलग-अलग राज्य बने थे .. जिनका हैदराबाद में संयुक्त उच्च-न्यायालय था। अब हैदराबाद उच्च-न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। उच्च न्यायालय एक राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है और एक राज्य के अन्य सभी न्यायालय उसके अधीन होते हैं।
रचना (Composition)-उच्च न्यायालयों के गठन सम्बन्धी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 216 में हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या सम्बन्धित राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती।
उनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है; जैसे हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 85 निश्चित की गई जबकि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में कुल संख्या 13 निश्चित की गई है। काम की अधिकता होने पर एक उच्च न्यायालय में अधिक-से-अधिक दो वर्षों के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges) भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्च न्यायालय के किसी सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए प्रार्थना कर सकता है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति-अनुच्छेद 223 के अन्तर्गत यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अन्य किसी कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को उस पद के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अतिरिक्त तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224
(1) के अन्तर्गत यदि किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप में कार्य बढ़ गया है और राष्ट्रपति यह अनुभव करता है कि इस कार्य के लिए न्यायाधीशों की संख्या को अस्थायी रूप से बढ़ाना आवश्यक है तो वह उपयुक्त योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अधिक-से-अधिक दो वर्ष के लिए अतिरिक्त (Additional) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।
इसी प्रकार अनुच्छेद 224 (2) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उस काल के लिए कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। – न्यायाधीशों का दूसरे राज्यों के उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरण-अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित करने का अधिकार है।
उच्चतम न्यायालय ने एस०पी० गुप्ता बनाम रतभा सरकार 1981 (न्यायाधीश मामला) में कहा, “सरकार का उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का दूसरे राज्यों में तबादला करने का अधिकार पूर्णतः वैधानिक है।” इसके लिए सम्बन्धित न्यायाधीश की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायाधीशों के स्थानान्तरण केवल जनहित (Public Interest) में ही किए जा सकते हैं, उन्हें दण्ड देने के लिए नहीं। इसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश से प्रभावी सलाह (Effective Consultation) लिया जाना आवश्यक है।
योग्यताएँ-अनुच्छेद 217 (2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गई हैं-
(1) वह भारत का नागरिक हो,
(2) वह भारत में किसी न्याय के पद पर कम-से-कम पाँच वर्ष तक रह चुका हो। अथवा वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में निरन्तर दस वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो।
कार्यकाल-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष पूर्ण होने तक अपने पद पर रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त दी गई अवस्थाओं में कोई न्यायाधीश पद-मुक्त हो सकता है-
(1) यदि उसकी पदोन्नति करके उच्चतम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाए,
(2) यदि भ्रष्टाचार या अयोग्यता के आधार पर संसद अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से दोनों सदनों में अलग-अलग किन्तु संसद के एक ही सत्र (Session) में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे,
(3) स्वयं त्यागपत्र देने पर,
(4) अवकाश-प्राप्ति के पश्चात् वह अपने न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है।
वेतन-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को समस्त भारत में समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ₹ 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,25,000 मासिक वेतन व भत्ते तथा रहने के लिए बिना किराए का निवास स्थान मिलता है। नियुक्ति के बाद उनके वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों को वेतन संचित निधि में से दिया जाता है। वित्तीय आपातस्थिति में ही उनके वेतन में कमी की जा सकती है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भारत के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है
1. साधारण अधिकार क्षेत्र-अनुच्छेद 225 के द्वारा भारत के उच्च न्यायालयों को वे सभी अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं जो संविधान के लागू होने से पूर्व उच्च न्यायालयों को प्राप्त थे। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा इस संविधान द्वारा विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी समुचित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी वर्तमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय के प्रशासन के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियाँ, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने का तथा उस न्यायालय की बैठकों की शक्तियाँ वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले थीं।।
2. प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र-कई मुकद्दमे सीधे उच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालयों को आरम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं
(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन मूल अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी मामला उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय में भी लाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय को कई तरह के लेख (Writs)
जारी करने का अधिकार है; जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus),
परमादेश लेख (Writ of Mandamus)
प्रतिषेध लेख (Writ of Prohibition),
अधिकार पृच्छा लेख (Writ of Quo-warranto),
उत्प्रेषण लेख (Writ of Certiorari),
(2) यदि राज्य विधान-मण्डल ने कोई कानून संविधान के विरुद्ध बनाया है तो उसको उच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। यद्यपि उसके फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है,
(3) तलाक, विवाह, वसीयत, न्यायालय का अपमान, . कम्पनी कानून आदि के मुकद्दमे भी उच्च न्यायालय द्वारा सीधे सुने जाते हैं,
(4) यदि उच्च न्यायालय ठीक समझे तो अधीनस्थ न्यायालयों से कोई मुकद्दमा सीधे अपने पास मंगवाकर उसकी सुनवाई कर सकता है,
(5) चुनाव सम्बन्धी मामले भी उच्च न्यायालय में सीधे लाए जाते हैं,
(6) मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता के उच्च न्यायालयों को कुछ अधिक प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
3. अपीलीय अधिकार क्षेत्र-उच्च न्यायालयों को निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी अभियोगों में अपीलें सुनने का अधिकार भी प्राप्त है-
(1) जिस मुकद्दमे में पाँच हजार या उससे अधिक राशि अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति का प्रश्न हो तो ऐसे दीवानी मुकद्दमों की अपील उच्च न्यायालय द्वारा सुनी जा सकती है,
(2) फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, यदि न्यायालय ने अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक कैद की सजा दी है,
(3) यदि अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दिया गया है,
(4) दीवानी क्षेत्र में पेटेन्ट (Patent) तथा डिज़ाइन (Design) उत्तराधिकार, भूमि-प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में उच्च न्यायालय अपील सुन सकता है,
(5) राजस्व सम्बन्धी मामलों में निम्न न्यायालयों और आय कर से सम्बन्धित मामलों में आय-कर अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनी जा सकती हैं।
4. प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र-देश के उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्य में अधीनस्थ सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों . पर निरीक्षण (Superintendence) का अधिकार है। 42वें संशोधन ने उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से अधिकरणों को निकाल , दिया था, किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 227 में संशोधन करके न्यायाधिकरणों को पुनः उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों पर अपना पूर्ण नियन्त्रण रखता है। यह नियन्त्रण इस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है-
- कार्रवाई का विवरण माँग सकता है,
- अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, अवकाश की शर्ते आदि निश्चित करता है,
- निम्न न्यायालय उच्च न्यायालय की इच्छानुसार तथा आदेश-निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं,
- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के कागजात माँगकर जाँच-पड़ताल कर सकता है,
- उनके रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था कर सकता है,
- किसी एक न्यायालय में किसी एक मुकद्दमे को हटाकर दूसरे अधीनस्थ न्यायालयों में विचार के लिए भेज सकता है।
5. न्यायिक पुनरावलोकन-उच्चतम न्यायालय की तरह राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। विधानसभा द्वारा पारित कानून यदि संविधान के निश्चित नियमों के विरुद्ध हो तो उच्च न्यायालय के सामने मुकद्दमा आने पर अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए वह उस कानून को गैर-कानूनी घोषित कर सकता है। उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
6. प्रमाण-पत्र देने का अधिकार उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है. यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करे। विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रमाण-पत्र के बिना भी अपील की अनुमति दे सकता है।
7. अभियोगों को स्थानान्तरित करना यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि किसी निम्न न्यायालय में चल रहे अभियोग में कानून की व्याख्या की आवश्यकता है अथवा अभियुक्त को किसी कारण पूरा न्याय मिलने की आशा नहीं है तो उच्च न्यायालय मुकद्दमा अपने पास मँगवा सकता है अथवा किसी दूसरे न्यायालय में भेज सकता है अथवा कानून की व्याख्या कर सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय को उच्च न्यायालय की व्याख्या को ध्यान में रखकर निर्णय करना पड़ता है।
8. अभिलेख न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय भी होता है। उसके सभी निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है तथा उन्हें प्रकाशित किया जाता है। इसमें निर्णय दृष्टान्त के रूप में विभिन्न आदेश में पेश किए जाते हैं। उच्च न्यायालय अपनी अवमानना करने (Contempt of Court) के लिए भी किसी व्यक्ति को दण्ड दे सकता है। उच्च न्यायालय की स्थिति-उच्च न्यायालय (High Court) न्यायिक मामलों में राज्य का उच्चतम न्यायालय है।
उसे प्रारम्भिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ-साथ मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में कई प्रकार के लेख (Writ) जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वह कार्यपालिका को नियन्त्रित करता है। उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के अधीन संसद व राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। राज्य के अन्य अधीनस्थ न्यायालय उसके नियन्त्रण में होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय न्यायिक शक्ति का शिखर नहीं है। उसके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

प्रश्न 6.
भारतीय न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर एक निबन्ध लिखें।
अथवा
उच्चतम न्यायालय की स्वतन्त्रता पर एक लेख लिखें।
उत्तर:
लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, ताकि कानून के शासन को बनाए रख सके तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। संघात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में स्वतन्त्र भूमिका और भी बढ़ जाती है। न्यायपालिका ही इस बात की गारन्टी करती है कि संघीय सरकार व राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में ही रहें। संविधान की सर्वोच्चता को स्वतन्त्र न्यायपालिका ही बनाए रख सकती है।
अर्थ-न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कार्यपालिका अथवा विधायिका न्यायाधीशों के निर्णयों को प्रभावित अथवा दुष्प्रभावित न कर सके। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से अभिप्राय है कि न्यायाधीश अपने निर्णय निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से देने की स्थिति में हों, उन्हें कोई प्रभावित कर सकने की स्थिति में न हो। भारतीय संविधान-निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान संविधान में किए हैं
1. न्यायाधीशों की नियुक्ति-संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की सलाह करके (जिन्हें वह सलाह लेने के उपयुक्त समझता है) करता है, और उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में जनता अथवा विधायिका की कोई भूमिका नहीं है। यद्यपि संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण सलाह अवश्य करता है, लेकिन वह न्यायाधीशों की सलाह की आमतौर पर उपेक्षा नहीं कर पाता है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका अधिक प्रभावी है, न कि कार्यपालिका अथवा विधायिका।
2. न्यायाधीशों की योग्यता संविधान में ही न्यायाधीशों की योग्यता निर्धारित की गई है, ताकि केवल अनुभवी विधि-विशेषज्ञ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सकें और सरकार मनमाने राजनीतिक आधार पर किसी को भी न्यायाधीश नियुक्ति न कर सके। एक उच्च कोटि के विद्वान् से सदैव यह आशा की जाती है कि वह अपना कार्य स्वतन्त्रता-पूर्वक व निर्भीक होकर करता है, उसे कोई सरकार प्रभावित नहीं कर सकती।
3. लम्बी अवधि-न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कार्य-अवधि लम्बी रखी गई है, जबकि सामान्यतया सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
4. पद की सुरक्षा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी जटिल पद्धति से ही हटाया जा सकता है। इसके लिए न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार (बरा व्यवहार) अथवा अयोग्यता का आरोप स्वतन्त्र व निष्पक्ष जाँच-पड़ताल द्वारा सिद्ध करना होता है
और उसके बाद संसद के दोनों सदन अपने-अपने सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। महाभियोग की इस प्रक्रिया की जटिलता का ज्ञान इसी तथ्य से हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी आरोप-पत्र 1990 में 101 सांसदों ने दिया था, जिस पर अभी तक विवाद चल रहा । है और महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भी नहीं हो पाई है।
5. वेतन व भत्तों की सुरक्षा संविधान में ही न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों की सुरक्षा की गई है। संसद न्यायाधीशों के . कार्यकाल के दौरान उनके वेतन व भत्तों में कटौती नहीं कर सकती, हाँ, बढ़ा अवश्य सकती है। भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं जिस पर संसद की स्वीकृति मात्र औपचारिकता होती है। न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में केवल वित्तीय संकट के दौरान ही कटौती की जा सकती है।
6. कर्मचारी वर्ग पर नियन्त्रण उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के अन्य सभी कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है और उन पर उच्चतम न्यायालय का नियन्त्रण होता है, न कि सरकार का।
7. नियम बनाना-उच्चतम न्यायालय अपनी कार्य प्रणाली के लिए संसदीय कानूनों के अनुसार नियम स्वयं बनाता है। नियमों के बनाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन ये नियम उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ भारत के अन्य सभी न्यायालयों में मान्य होते हैं।
8. अवकाश-प्राप्ति के बाद वकालत की मनाही-न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में ही व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष बन सकता है।
9. उन्मुक्तियाँ-न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को कुछ उन्मुक्तियाँ व विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे न्यायाधीशों की आलोचना उनके द्वारा किए गए निर्णयों के कारण नहीं की जा सकती। संसद न्यायाधीशों के ऐसे कार्यों . पर, जिसे उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए किया है, विचार-विमर्श नहीं कर सकती। धान-निर्माताओं ने व्यापक व विस्तृत रूप से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, लेकिन व्यवहार में ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हैं जिनसे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न हुआ है।
प्रश्न 7.
न्यायिक क्रियाशीलता से आपका क्या तात्पर्य है? इसके मुख्य साधनों की व्याख्या करो।
उत्तर:
सरकार के तीन महत्त्वपूर्ण अंग-विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका हैं। विधानपालिका कानून बनाने, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने तथा न्यायपालिका निर्णय देने का कार्य करती है। मान्टेस्क्यू ने शक्ति विभाजन के सिद्धान्त में यह बताया है कि इन तीनों अंगों को अपने उप-क्षेत्र में काम करना चाहिए तथा एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार के तीनों अंग अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं और एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने कार्यपालिका व विधानपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है और इसी हस्तक्षेप को विभिन्न कानूनवेताओं, राजनीतिकों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने न्यायिक क्रियाशीलता का नाम दिया है।
न्यायिक क्रियाशीलता का अर्थ (Meaning of Judicial Activism) न्यायिक क्रियाशीलता भारत में एक नवीन अवधारणा है। इसलिए इसकी ठीक ढंग से व्याख्या करना कठिन है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य निर्णय देना है। जब निर्णय संविधान अथवा कानून के अनुसार दिए जाते हैं तो इसे न्यायिक क्रियाशीलता का नाम नहीं दिया जाता। परन्तु जब न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधानपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करती है तब इसे न्यायिक क्रियाशीलता कहा जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों को निश्चित कर और उन्हें लागू करने के आदेश देना। योजनाओं के संचालन को अपने हाथ में लेना, स्वाधीन संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप करना।
कानून का निर्माण करने के लिए विधानपालिका को निर्देश देना आदि, न्यायिक क्रियाशीलता के प्रतीक माने जाते हैं। साधारण शब्दों में, न्यायपालिका की किसी भी कार्रवाई को न्यायिक क्रियाशीलता की संज्ञा दी जा सकती है। जिसके द्वारा न्यायपालिका की प्राथमिकता स्थापित होती है। अतः न्यायिक क्रियाशीलता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में क्रियाशील भूमिका निभाना न होकर क्षेत्राधिकार से बाहर क्रियाशील भूमिका निभाने व कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पी०बी० सावंत (P.B. Swant) के शब्दों में, “कानून की व्याख्या करने और इसे लागू करते समय सवैधानिक सीमा की अवहेलना करना, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए विधानपालिका के कार्यों को अपने हाथ में लेने को न्यायिक क्रियाशीलता कहा जाता है।”
न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता (Need of Judicial Activism)-प्रशासन एक इकाई है सरकार के तीनों अंग अलग-अलग होते हुए मिलकर कार्य करते हैं तभी एक योग्य प्रशासन सम्भव होता है, परन्तु जब सरकार अपने दायित्वों को निभाने में ढीलापन अथवा अनियमितता दिखाता है, तब कानून का शासन स्थापित करना कठिन हो जाता है। हर तरफ भ्रष्टाचार फैल जाता है। नौकरशाही तथा राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी विशिष्ट स्थिति का गलत प्रयोग किया जाता है और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं अर्थात् एक तरह का जंगल राज होता है।
ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को क्रियाशील होना ही पड़ता है। न्यायमूर्ति जे०एस० वर्मा के शब्दों में, “न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता केवल तब ही होती है जब अन्य अक्रियाशील होते हैं। एक स्थान पर जे०एस० वर्मा ने फिर कहा है, “न्यायिक क्रियाशीलता अक्रियाशीलता को क्रियाशील बनाती है।” अतः दूसरों की अक्रियाशीलता ही न्यायिक क्रियाशीलता को जन्म देती है। न्यायिक क्रियाशीलता के साधन (Means (Devices) of Judicial Activism)-न्यायिक क्रियाशीलता के साधन निम्नलिखित हैं
1. न्यायिक पुनर्निरीक्षण-न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति न्यायिक क्रियाशीलता का प्रथम व महत्त्वपूर्ण साधन है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के अधीन सर्वोच्च न्यायालयों व उच्च न्यायालयों को उन कानूनों व कार्यपालिका के आदेशों को रद्द करने का अधिकार है जो संविधान की इच्छा के विरुद्ध है। न्यायपालिका न्यायिक पुनर्निरीक्षण से ऐसे सिद्धान्त निश्चित करती है जो सरकार के अन्य अंगों पर बाध्यकारी होते हैं। इस तरह न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायिक क्रियाशीलता का एक साधन है; जैसे 1973 का केशवानन्द भारती का मुकद्दमा।
2. मौलिक अधिकारों की व्याख्या-न्यायिक क्रियाशीलता का द्वितीय साधन मौलिक अधिकार की व्याख्या है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा धारा 31 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति मौलिक अधिकारों की अवहेलना होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने-अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है।
न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करते समय कुछ ऐसे निर्देश जारी करती है जो न्यायिक क्रियाशीलता का उदाहरण होते हैं; जैसे 4 फरवरी, 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय बालक का मौलिक अधिकार है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय संविधान धारा 21 की नई व्याख्या न्यायिक क्रियाशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।
3. कानून निर्माण साधारणतः कानून निर्माण न्यायपालिका का कार्य नहीं है, परन्तु अनेक बार न्यायपालिका कानून निर्माण भी करती है जो न्यायिक क्रियाशीलता का स्पष्ट उदाहरण है; जैसे कई बार न्यायपालिका के समक्ष ऐसा विचित्र झगड़ा पेश होता है जिस पर विधानपालिका का कोई कानून नहीं तो न्यायाधीश अपनी सूझ-बूझ, अनुभव तथा योग्यता के आधार पर जो निर्णय कर देते हैं वह कानून का एक अंग बन जाता है। न्यायाधीशों द्वारा इस प्रकार दिए गए निर्णयों को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून (Judge Maker) या केस लॉ (Case Law) कहा जाता है ये निर्णय न्यायिक प्रमाण (Judicial Precedent) बन जाते हैं और अन्य न्यायालयों पर भी बाध्य होते हैं। ऐसे निर्णय न्यायपालिका की क्रियाशीलता के उदाहरण है।
4. संविधान की व्याख्या न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। लिखित संविधान में संविधान की अनेक धाराओं से सम्बन्धित अंतिम व्याख्या न्यायपालिका का दायित्व होता है। संविधान की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय नवीन कानून सिद्धान्त, नियम व विधियाँ आदि निर्धारित करती हैजैसे 6 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को कार्यपालिका की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। अतः संविधान की व्याख्या न्यायिक क्रियाशीलता का एक अन्य साधन है।
5. सार्वजनिक हित के लिए मुकद्दमेबाजी-सार्वजनिक हित के लिए मुकद्दमेबाजी न्यायिक क्रियाशीलता का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। साधारणतः कानून के अन्तर्गत के केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्यायालय में मुकद्दमा कर सकते हैं। दूसरे किसी व्यक्ति को मुकद्दमा दायर करने का अधिकार नहीं है, परन्तु सार्वजनिक हित के मुकद्दमेबाजी में कोई व्यक्ति सार्वजनिक विषय के सम्बन्ध में न्यायालय में मुकद्दमा दायर कर सकता है तथा उस मुकद्दमे से उस व्यक्ति का सम्बन्धित होना आवश्यक नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 (क) वह स्रोत है जो सार्वजनिक हित के विवादों की अवधारणा को पर्याप्त सीमा तक मान्यता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित के न्याय के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यदि कोई व्यक्ति पोस्ट कार्ड पर भी आवेदन-पत्र लिखकर या अन्याय की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में करता है तो शिकायत दर्ज हो जाती है; जैसे कमजोर वर्ग, मज़दूरों, स्त्रियों व बच्चों की शिकायतों को विशेष महत्त्व दिया जाता है।
निष्कर्ष-भारत में न्यायिक क्रियाशीलता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ इसके पक्ष में और अन्य इसके विपक्ष में हैं। भारत में न्यायिक क्रियाशीलता का महत्त्वपूर्ण साधन सार्वजनिक हित के सम्बन्ध में मुकद्दमेबाजी है। इसमें न्यायालय कार्यपालिका सरकार को या संस्थाओं को कुछ ऐसे आदेश या निर्देश देती है जो उन्हें मानने पड़ते हैं न मानने पर न्यायपालिका की अवहेलना होने का डर है। न्यायिक क्रियाशीलता में असंख्य पीड़ित बालकों, स्त्रियों व श्रमिकों को लाभ हुआ है। न्यायिक क्रियाशीलता से समाज की कई बुराइयों का अन्त भी हुआ है; जैसे बन्धुआ मजदूरी का अन्त आदि।
प्रश्न 8.
न्यायपालिका की सक्रियता के कारणों या तत्त्वों का वर्णन करो।
उत्तर:
न्यायिक क्रियाशीलता के तत्त्व या कारण (Causes or Elements of Judicial Activism)-संवैधानिक रूप में न्यायिक क्रियाशीलता का केवल एक ही तत्त्व-न्यायिक पुनर्निरीक्षण है, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्त्व भी हैं जिन्होंने न्यायिक क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया है। ऐसे तत्त्वों का विवरण निम्नलिखित है
1. यदि प्रत्येक व्यक्ति या विभाग अपने दायित्वों को निभाता रहे तो दूसरे के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। किसी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता तब अवश्य हो जाती है जब कोई अपने दायित्वों को नहीं निभाता। ऐसा न्यायपालिका की स्थिति में हुआ है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप उसकी कर्त्तव्य विमुखता और पथ भ्रमिता के कारण किया। कार्यपालिका न केवल केन्द्रीय स्तर पर, बल्कि राज्य स्तर पर भी अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रही है। कार्यपालिका के इस कर्त्तव्य न निभाने की प्रवृत्ति ने लोगों को हताश कर दिया है।
अतः न्यायक्रियाशीलता का प्रारम्भ हुआ। कार्यपालिका की अक्रियाशीलता के कारण न्यायपालिका की क्रियाशीलता के लिए यह उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब सन् 1994 में उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे तो आन्दोलन के दौरान प्रशासन द्वारा उन पर अत्याचार किए गए। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ भी घटीं। परन्तु राज्य व केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में जाँच के आदेश दिए। इसी प्रकार बिहार में चारा घोटाला के मामले में भी राज्य सरकार को वहाँ के उच्च न्यायालय ने ही जाँच के आदेश दिए। अतः स्पष्ट है कि कार्यपालिका की अनदेखी अक्रियाशीलता ही न्यायिक क्रियाशीलता का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
2. जनहित मुकद्दमे-जनहित के मुकद्दमे भी न्यायिक क्रियाशीलता का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। साधारणतः व्यक्ति अपने हित की रक्षा हेतु ही मुकद्दमा कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए नहीं। इस प्रकार कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित की प्राप्ति के लिए कोई मुकद्दमा नहीं लड़ सकता। परन्तु हाल ही में जनहित के मुकद्दमों की धारणा सामने आई है।
जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति या वर्ग किसी कारण से हितों या अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके अधिकारों या हितों की रक्षा के लिए मुकद्दमा डालने का अधिकार है। जनहित की पद्धति का आरम्भ न्यायमूर्ति श्री० पी०एन० भगवती ने किया इस पद्धति ने गरीब, अनपढ़ और अनजान लोगों के लिए न्याय का रास्ता खोला है। अतः स्पष्ट है कि जनहित के मुकद्दमों ने न्यायिक क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाना, शहरी आवास आबंटन घोटाला, बिहार (भागलपुर) क्षेत्र के मामले, श्रमिकों के शोषण के मामले आदि जनहित मुकद्दमों के कतिपय उदाहरण हैं।
3. स्वतन्त्र न्यायपालिका-न्यायपालिका की स्वतन्त्रता भी न्यायिक क्रियाशीलता का महत्त्वपूर्ण तत्त्व या कारण है। स्वतन्त्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायपालिका पर कोई आन्तरिक व बाह्य दबाव नहीं होता। न्यायपालिका निर्भीकता से कार्य करती है। इससे न्यायपालिका की कार्यशीलता बढ़ती है। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतन्त्र रूप से किसी भी बड़े-से-बड़े पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि कर्त्तव्यपरायण, निर्भीक और प्रखर न्यायाधीश ही न्यायपालिका को सक्रियता प्रदान कर सकते हैं।
4. जनता का कार्यपालिका के प्रति घटता विश्वास जनता के कार्यपालिका के प्रति घटते विश्वास ने भी न्यायिक क्रियाशीलता को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उसको बढ़ावा भी दिया है। पिछले दशक में न्यायिक अस्थिरता ने कार्यपालिका के प्रति जनता के विश्वास को घटाया है और वह निरन्तर घटता ही जा रहा है। इसके विपरीत न्यायपालिका ने कार्यपालिका को उसकी कर्तव्य विमुखता उदासीनता के लिए चेतावनी दी है जिससे आम जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है और आम जनता विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधारों के लिए न्यायपालिका से आशा लगाए बैठी है। यही नहीं न्यायपालिका ने जनता के दुःख-दर्द को पहचाना है और उसे दूर करने के लिए अपने दायित्व को निभाया है। अतः इससे न्यायिक क्रियाशीलता का बढ़ना स्वाभावि न्यायिक पनर्निरीक्षण की शक्ति-न्यायिक क्रियाशीलता का एक और महत्त्वपूर्ण कारण है-न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति।
5. भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध बने कानूनों को रद्द कर सकती है। इससे न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में भी न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का सही अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेक मामलों में न्यायपालिका ने संविधान की व संघात्मक व्यवस्था की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करके न्यायिक क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया है।
6. राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता भी न्यायिक क्रियाशीलता या न्यायिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण कारण है। कभी एक समान या संसद में एक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता था और सरकार स्थायी व सुचारू रूप से कार्य करती थी, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से संसद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप साँझा सरकारें बनी हैं। साँझा सरकार में निश्चित रूप से सरकार की गुणात्मक शक्ति को धक्का लगा है। संसद की क्रियात्मक शक्तियों का ह्रास हुआ है। अतः संसद की शक्ति कमजोर होने से न्यायपालिका की शक्तियों को बढ़ावा मिला है। जिसे न्यायिक क्रियाशीलता ही कहा जा सकता है।
7. राजनीतिक नेताओं की छलिया राजनीति राजनीतिक नेताओं की छलिया राजनीति ने भी न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। राजनीतिक नेताओं की कपटी गतिविधियों के कारण न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कई बार तो न्यायपालिका को न चाहते हुए भी क्रियाशील होना पड़ता है। आजकल राजनीतिक नेता जिन मामलों को स्वयं सुलझा नहीं सकते हैं और जिन मामलों को सुलझाने में बुराई या भलाई दोनों मिल सकती है तो
इसलिए वे बुराई मिलने के भय से उस मामले को सुलझाने का दायित्व न्यायपालिका पर छोड़ देते हैं। जिससे राजनीतिक नेता साफ बच जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका को सक्रिय होने पर विवश कर देते हैं। उपर्यक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि न्यायिक क्रियाशीलता के कई कारण हैं और इन कारणों या तत्त्वों ने न्यायपालिका को सक्रिय होने में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, जिनसे न्यायिक क्रियाशीलता के बढ़ने की अधिक सम्भावना है।
प्रश्न 9.
न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। अथवा न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। अथवा न्यायिक क्रियाशीलता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
सामान्यतः संसदीय जनतन्त्र में संसद को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है किन्तु भारत में यही बात संविधान के ऊपर लागू होती है। यहाँ संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और न्यायपालिका अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के बल पर संसद से उच्च सिद्ध हो जाती है। हालाँकि भारतीय संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
किन्तु वहीं पर इस बात का उल्लेख अवश्य मिलता है कि यदि कोई भी क्रिया-कलाप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे संवैधानिक घोषित किया जा सकता है और इस घोषणा को करने का अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका को प्राप्त है।
आरम्भ में न्यायपालिका का यह अधिकार सिर्फ इस बात की समीक्षा तक ही सीमित था कि कार्यपालिका अथवा विधायिका द्वारा लिए गए किसी निर्णय अथवा उठाए गए किसी कदम से कहीं मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है किन्तु धीरे-धीरे न्यायपालिका ने अपने इस अधिकार का विस्तार करना शुरु कर दिया और सामाजिक मुद्दों से जुड़े सवालों, पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं तथा जनताँत्रिक संगठनों के क्रिया-कलापों की भी समीक्षा करनी प्रारम्भ कर दी। न्यायपालिका की इसी सक्रियता को न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है।
न्यायिक क्रियाशीलता के विपक्ष में तर्क (Arguments in Against of Judicial Activism)-न्यायिक क्रियाशीलता की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है
1. यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है-शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुसार सरकार के तीनों अंग अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं। विधानपालिका कानून बनाने, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने तथा न्यायपालिका निर्णय देने का कार्य करती है। किसी भी अंग को दूसरे अंग के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता तथा हस्तक्षेप असवैध माना जाता है।
संविधान में न्यायपालिका को एक सीमा तक विधानपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है, यदि विधानपालिका संविधान की इच्छा के विरुद्ध कानून बनाती है, तब न्यायपालिका को ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु न्यायिक क्रियाशीलता में न्यायपालिका अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर विधानपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। परिणामस्वरूप सरकार के सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न होती है, अतः न्यायिक क्रियाशीलता शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है।
2. उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के विरुद्ध न्यायिक क्रियाशीलता की आलोचना उत्तरदायित्व की अवधारणा के विरुद्ध है। उत्तरदायित्व की अवधारणा का अर्थ है कि किसी का किसी के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों लोगों के प्रति उत्तरदायी है। लोग विधानपालिका और कार्यपालिका दोनों का समय-समय पर मूल्याँकन करते रहते हैं; जैसे मन्त्रिमण्डल लोगों द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति अपने क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है।
मन्त्रिमण्डल तभी तक सत्ता में रह सकता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त होता है। इसी प्रकार विधानपालिका अर्थात् संसद के सदस्य भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जनता ऐसे सांसदों का दुबारा निर्वाचित नहीं करती जो उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते अर्थात् मन्त्रियों और सांसदों के लिए दोबारा चुनाव जीतना कठिन हो जाता है, जो लोगों की आशाओं पर पूर्ण नहीं उतरते हैं, परन्तु न्यायपालिका विधानपालिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
यहाँ तक न्यायाधीश भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। न्यायपालिका न्यायिक क्रियाशीलता में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं। इस प्रकार अनुत्तरदायित्व की भावना से न्यायपालिका अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर लेती है वैसे भी एक अनुत्तरदायी संस्था उत्तरदायी संस्थाओं को आदेश दे, यह अनुचित है।
3. संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध न्यायिक क्रियाशीलता को संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध मानकर उसकी आलोचना की जाती है। संसदीय व्यवस्था में कानून बनाने का कार्य विधानपालिका करती है। न्यायपालिका को संविधान द्वारा केवल यह अधिकार दिया गया है कि विधानपालिका द्वारा संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करें।
न्यायपालिका को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन न्यायिक क्रियाशीलता के अन्तर्गत न्यायपालिका ने तो संसद को कानून बनाने के आदेश देने आरम्भ कर दिए हैं। न्यायपालिका विधानपालिका का तीसरा सदन बनने का प्रयत्न कर रही है जो संसदीय व्यवस्था की आत्मा के विरुद्ध है अर्थात न्यायिक क्रियाशीलता ससंदीय लोकतन्त्र की कार्य-प्रणाली पर बुरा प्रभाव डालेगी।
4. न्यायपालिका के कार्यों पर कुप्रभाव न्यायिक क्रियाशीलता की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि यह न्यायपालिका की दैनिक कार्य-प्रणाली पर बुरा प्रभाव डालती है। न्यायिक क्रियाशीलता सार्वजनिक हित के मुकद्दमेबाजी को प्रोत्साहन देती है। न्यायिक क्रियाशीलता से न्यायपालिका ने सार्वजनिक हित के मुकद्दमों का अम्बार लग जाएगा, न्यायालय या उच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित के मुकद्दमे को ले जाना आसान हो गया है।
इस प्रकार यह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में वृद्धि कर देगी, जबकि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही अधिक काम के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। आज की तिथि में भी लाखों मुकद्दमें न्यायालयों में पड़े हुए हैं जिनको समय के अभाव के कारण से निपटाया नहीं जा सका है। न्यायिक क्रियाशीलता न्यायपालिका के दैनिक कार्यों को भी और बढ़ा देगी जिससे न्यायपालिका की कार्य-प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
5. प्रजातन्त्र के विरुद्ध-न्यायिक क्रियाशीलता को प्रजातन्त्र के विरुद्ध माना जाता है। प्रजातन्त्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है तथा ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। साथ ही प्रशासन एक कला है जिसे केवल प्रशासनिक कला में माहिर लोगों के द्वारा ही चलाया जा सकता है। माना न्यायाधीश द्धजीवी होते हैं परन्तु वे कानून के क्षेत्र में ही माहिर होते हैं। प्रशासन से उनका कुछ लेना-देना नहीं होता।
इसलिए यदि न्यायाधीश न्यायिक क्रियाशीलता के अन्तर्गत प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तो यह उचित नहीं होगा और साथ में यह प्रजातन्त्र विरोधी भी होगा क्योंकि प्रशासन चलाना प्रशासकों का काम है न कि न्यायाधीशों का। हाँ यदि प्रशासन दोषपूर्ण है तो कानून द्वारा उसमें सुधार करवाने के लिए न्यायपालिका अवश्य ही सकारात्मक भूमिका निभा सकती है परन्तु न्यायिक क्रियाशीलता द्वारा शासन को अपने हाथों में लेना निश्चित रूप से प्रजातन्त्र के विरुद्ध है।
6. न्यायिक निरंकुशता को प्रोत्साहन-न्यायिक क्रियाशीलता की इस आधार पर भी आलोचना की जा सकती है कि यह न्यायिक निरंकुशता को प्रोत्साहित करती है। न्यायिक क्रियाशीलता से न्यायपालिका की निरंकुशता स्थापित होने का भय बना रहता है। न्यायिक क्रियाशीलता यहाँ तक तो सही है कि यह विधानपालिका और कार्यपालिका को अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगाह करती है।
परन्तु एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि यदि न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती तो उसे कौन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहेगा। न्यायपालिका के कार्यों को कौन असंवैधानिक घोषित करेगा अर्थात् न्यायपालिका पर कोई अंकुश नहीं है और उसके निरंकुश बनने की पूरी सम्भावना है। अतः न्यायपालिका की निरंकुशता भी अन्य निरंकुशताओं की तरह होगी, जिसमें लोगों के अधिकार छीन लिए जाएँगें परन्तु लोग न्यायपालिका की निरंकुशता को सहन नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठेंगे।
न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Judicial Activism)-न्यायिक क्रियाशीलता के विपक्ष . में तर्क देखने के पश्चात् ऐसा लगता है कि न्यायिक क्रियाशीलता अनुचित है परन्तु न्यायिक क्रियाशीलता ने भारतीय राजनीति को कई प्रकार से प्रभावित किया है इसलिए न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। इन तर्कों का विवरण निम्नलिखित है
1. सरकार को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में प्रथम और महत्त्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि यह सरकार के विभिन्न अंगों को सक्रिय बनाने में सहायता करती है। साधारणतः यह देखा गया है कि सरकार के अंग विधानपालिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो जाते हैं।
भारत का अब तक का इतिहास इस बात का गवाह है कि कार्यपालिका, विधानपालिका व अन्य संस्थाओं ने अपने कर्तव्यों की ओर से मुँह मोड़ लिया था। वह अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से नहीं निभा रहे थे। काफी समय तक न्यायपालिका ने इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया परन्तु कुछ वर्षों से न्यायपालिका ने इस अक्रियाशीलता के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है और उसके हस्तक्षेप से बहुत से घोटाले सामने आए हैं। यही नहीं कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। अतः स्पष्ट है कि न्यायिक क्रियाशीलता से सरकार की क्रियाशीलता को सक्रिय बनाया जा सकता है।
2. राजनीतिक प्रणाली की सही स्थिति जानने में सहायक-न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में एक और तर्क यह दिया जाता है कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली की क्रियाशीलता को जानने में या उसका सही रूप पहचानने में सहायता करती है। न्यायपालिका स्वतन्त्र होती है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका या विधानपालिका का किसी भी प्रकार से नियन्त्रण नहीं होता।
इसलिए न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानपालिका को निर्देश दे सकती है और उन्हें इसके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। न्यायपालिका की क्रियाशीलता से अनेक घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार सामने आए हैं। न्यायपालिका की क्रियाशीलता के कारण ही लोगों को हैरान कर देने वाली बातों का पता लगा है। अतः स्पष्ट है कि न्यायिक क्रियाशीलता की वजह से ही सरकार की अक्रियाशीलता और राजनीतिक प्रणाली का सही रूप देखने को मिलता है।
3. संविधान की सुरक्षा-न्यायिक कार्यशीलता के पक्ष में एक अन्य महत्त्वपूर्ण तर्क यह है कि यह संविधान की सुरक्षा करती है। यह कानून के शासन को स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। संविधान में विधानपालिका को अधिकार-क्षेत्र का वर्णन होता है और उसके लिए यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने-अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य करें।
यदि कार्यपालिका या विधानपालिका अपने अधिकार-क्षेत्र की अवहेलना करती है तो न्यायपालिका उनके ऐसे कार्यों को अवैध घोषित करके न्यायिक क्रियाशीलता का परिचय देती है। अतः स्पष्ट है कि कार्यपालिका और विधानपालिका द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में न्यायपालिका निर्देश दे सकती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कानून के शासन व संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता है।
4. कानूनों की व्याख्या में सहायक-न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में एक और तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे कानूनों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। यही नहीं कई बार क्रियाशील न्यायपालिका नए कानून बनाने और पुराने कानूनों की त्रुटियों को दूर करने में भी सहायता करती है। कानून साधारणतः विधानपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। विधानपालिका के सदस्य कानून-वेता नहीं होते, बल्कि साधारण व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा अस्पष्ट कानूनों का निर्माण किया जा सकता है।
कई बार कानूनों की भाषा इस प्रकार की होती है कि उसके एक में से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसी स्थिति में क्रियाशील न्यायपालिका ही कानूनों की सही व्याख्या करती है। यह कानूनों की त्रुटियों को दूर करने में सहायता करती है। क्रियाशील न्यायपालिका नवीन धारणाओं और कानूनों का जन्म देती है। अतः न्यायिक क्रियाशील के अभाव में कानूनों की त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता।
5. भावी कानूनों के निर्माण में सहायक निःसन्देह विधानपालिका मनुष्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है, परन्तु समय बदलता रहता है। कई बार जीवन में विचित्र प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई कानून नहीं होता। इसका अर्थ यह लगाना चाहिए जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक कोई निर्णय होगा।
ऐसी स्थिति में न्यायाधीश अपनी बुद्धिमता के अनुसार निर्णय देता है। वे अपनी न्याय भावना का प्रयोग करके अमुक मुकद्दमे का फैसला कर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में किसी प्रकार कानून बना नहीं होता। वहाँ न्यायिक क्रियाशीलता की सहायता से मामले को निपटा दिया जाता है। इस प्रकार न्यायिक क्रियाशीलता निर्णय करने में सहायता प्रदान करती है।
6. मानवीय अधिकारों की रक्षा में सहायक-न्यायिक क्रियाशीलता ने मानवीय अधिकारों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यायिक क्रियाशीलता के अभाव में गैर-कानूनी नज़रबन्दी बच्चों के शोषण के मामले, स्त्रियों के शोषण के मामले, स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के मामले आदि जनता के सामने नहीं आते। यद्यपि भारतीय संविधान में लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्राप्त है।
वे अधिकारों की अवहेलना की स्थिति में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, परन्तु कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम! क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं होते। धन के अभाव तथा जानकारी के अभाव में लोगों के अधिकारों का लगातार हनन होता रहता है। लेकिन न्यायिक क्रियाशीलता ने सार्वजनिक हित की मुकद्दमेबाजी (Public Interest Litigation) को जन्म दिया है जिसके द्वारा आम जनता के अधिकार की या मानवाधिकारों की रक्षा होती है।
7. लोगों का समर्थन-न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष में अन्तिम तर्क यदि दिया जा सकता है कि इसे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। लोगों ने हार्दिक दिल से न्यायिक क्रियाशीलता का समर्थन किया है। क्योंकि इसके कारण बहुत से घोटाले, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के कारनामें, उच्च अधिकारियों की वास्तविक तस्वीर सामने आई है। आम जनता कार्यपालिका व नौकरशाही की लाल फीताशाही से तंग आ चुकी थी। केवल न्यायिक क्रियाशीलता ने लोगों को एक निष्पक्षता की किरण दिखाई। जनता ने यह समझ लिया है कि न्यायपालिका की क्रियाशीलता ही उन्हें भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और अधिकारियों से छुटकारा दिला सकती है।
निष्कर्ष-न्यायिक क्रियाशीलता के पक्ष व विपक्ष के तकों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत जैसे विकासशील देश में न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता है। भारत के विगत वर्षों के प्रशासन ने यह साबित कर दिया है कि भारत में नौकरशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। राजनीतिक नेताओं ने जनता की सहायता करने की बजाय अपने घरों को भरने का प्रयत्न किया है।
अतः वर्तमान स्थिति में न्यायिक क्रियाशीलता की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि बढ़ते भ्रष्टाचार व नौकरशाही पर रोक लगाई जा सके, परन्तु जहाँ जरूरत हो वहाँ न्यायिक क्रियाशीलता पर रोक की भी आवश्यकता है। न्यायपालिका को केवल सरकार के दूसरे अंगों को क्रियाशील बनाने में आवश्यक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए परन्तु स्वयं अधिक क्रियाशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की न्यायिक क्रियाशीलता न्यायपालिका की निरंकुशता को जन्म दे सकती है तथा निरंकुशता तो किसी की भी क्यों न हो, अच्छी नहीं होती।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें
1. निम्नलिखित में से न्यायपालिका का कार्य है
(A) कानूनों को लागू करना
(B) चोरों को पकड़ना
(C) खेती को बढ़ावा देना
(D) झगड़ों का निपटारा करना
उत्तर:
(D) झगड़ों का निपटारा करना
2. निम्नलिखित में से न्यायपालिका का कार्य नहीं है
(A) मुकद्दमों का फैसला करना
(B) अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना
(C) कानूनों की व्याख्या करना
(D) नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना
उत्तर:
(B) अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है
(A) लोकतंत्र की रक्षा के लिए
(B) संविधान के संरक्षण के लिए
(C) नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी

4. निम्नलिखित न्यायपालिका की स्वतंत्रता का साधन है
(A) न्यायाधीशों की नियुक्ति का उचित तरीका
(B) अच्छे वेतन
(C) न्यायाधीशों को पद से हटाने का कठिन तरीका
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?
(A) 30
(B) 26
(C) 31
(D) 34
उत्तर:
(D) 34
6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है
(A) प्रधानमन्त्री
(B) उप-राष्ट्रपति
(C) राष्ट्रपति
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) राष्ट्रपति
7. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं
(A) 62 वर्ष
(B) 65 वर्ष
(C) 70 वर्ष
(D) 60 वर्ष
उत्तर:
(B) 65 वर्ष
8. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है
(A) ₹ 1,00,000
(B) ₹ 2,50,000
(C) ₹ 2,80,000
(D) ₹ 1,25,000
उत्तर:
(C) ₹ 2,80,000
9. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मासिक वेतन मिलता है
(A) ₹ 1,00,000
(B) ₹ 90,000
(C) ₹ 1,50,000
(D) ₹2,50,000
उत्तर:
(D) ₹ 2,50,000
10. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है
(A) लोकसभा अध्यक्ष को
(B) राज्यसभा के अध्यक्ष को
(C) किसी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ को
(D) किसी प्रसिद्ध विधिवेत्ता को
उत्तर:
(D) किसी प्रसिद्ध विधिवेत्ता को
11. सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले सम्बन्धी कानूनी परामर्श ले सकता है
(A) प्रधानमन्त्री
(B) राष्ट्रपति
(C) उप-राष्ट्रपति
(D) लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर:
(B) राष्ट्रपति
12. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अन्तिम रक्षक कौन है?
(A) राष्ट्रपति
(B) उप-राष्ट्रपति
(C) संसद
(D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर:
(D) सर्वोच्च न्यायालय
13. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है
(A) संसद द्वारा
(B) संविधान द्वारा
(C) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(B) संविधान द्वारा
14. भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है?
(A) मुम्बई में
(B) चंडीगढ़ में
(C) नई दिल्ली में
(D) चेन्नई में
उत्तर:
(C) नई दिल्ली में
15. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है?
(A) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
(B) प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
(C) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(D) संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा
उत्तर:
(D) संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा
16. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए
(A) बाध्य है
(B) बाध्य नहीं है
(C) सीमित रूप से बाध्य है
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(B) बाध्य नहीं है
17. निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है?
(A) संसद
(B) राष्ट्रपति
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय
उत्तर:
(C) सर्वोच्च न्यायालय
18. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) संसद
(D) मुख्य न्यायाधीश
उत्तर:
(A) राष्ट्रपति
19. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं
(A) 58 वर्ष तक
(B) 60 वर्ष तक
(C) 62 वर्ष तक
(D) 65 वर्ष तक
उत्तर:
(D) 65 वर्ष तक
20. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है
(A) ₹ 1,00,000
(B) ₹ 2,50,000
(C) ₹ 2,80,000
(D) ₹ 1,50,000
उत्तर:
(B) ₹ 2,50,000
21. उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मासिक वेतन मिलता है
(A) ₹ 90,000
(B) ₹ 1,00,000
(C) ₹2,50,000
(D) ₹ 2,25,000
उत्तर:
(D) ₹ 2,25,000
22. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(A) सेवा-निवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं
(B) उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं
(C) सेवा-निवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकते
(D) 65 वर्ष से पूर्व हटाए नहीं जा सकते
उत्तर:
(C) सेवा-निवृत्त होने के बाद वकालत नहीं कर सकते
23. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला (Transfer) कर सकता है
(A) राष्ट्रपति
(B) राज्यपाल
(C) संसद
(D) मुख्यमंत्री
उत्तर:
(A) राष्ट्रपति
24. पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय स्थित है
(A) हिसार में
(B) पटियाला में
(C) अमृतसर में
(D) चंडीगढ़ में
उत्तर:
(D) चंडीगढ़ में
25. 23 अप्रैल, 2021 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? ।
(A) श्री दीपक मिश्रा
(B) श्री जगदीश सिंह खेहर
(C) श्री रंजन गोगोई
(D) श्री शरद अरविंद बोबड़े
उत्तर:
(D) श्री शरद अरविंद बोबड़े
26. उच्च न्यायालय का निम्नलिखित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है
(A) मौलिक अधिकार के मामले
(B) फौजदारी मामले
(C) अपीलें सुनना
(D) कानून निर्माण
उत्तर:
(A) मौलिक अधिकार के मामले
27. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है?
(A) राष्ट्रपति
(B) राज्यपाल
(C) प्रधानमंत्री
(D) संसद
उत्तर:
(D) संसद
28. भारत में इस समय कुल उच्च न्यायालय हैं
(A) 23
(B) 24
(C) 25
(D) 26
उत्तर:
(C)25
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें
1. किन्हीं ऐसे दो देशों के नाम बताएँ, जिनमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता।
उत्तर:
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं?
उत्तर:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस समय एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश (कुल 34) हैं।
3. भारत में इस समय कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
उत्तर:
भारत में इस समय कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
4. किन्हीं ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जिनका एक ही (साझा) उच्च न्यायालय है। वह कहाँ पर स्थित है?
उत्तर:
हरियाणा तथा पंजाब का एक ही साझा उच्च न्यायालय है जो चण्डीगढ़ में स्थित है।

5. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है ?
उत्तर:
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है।
6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है?
उत्तर:
अनुच्छेद 124 में।
7. सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी पूर्व अनुमति से की जा सकती है?
उत्तर:
राष्ट्रपति की।
8. संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु कितनी न्यूनतम आयु निश्चित की गई है?
उत्तर:
न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है।
9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से दिया जाता है?
उत्तर:
भारत की संचित निधि से।
10. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?
उत्तर:
राष्ट्रपति।
11. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
उत्तर:
65 वर्ष।
12. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या विधि है?
उत्तर:
महाभियोग विधि।
13. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
उत्तर:
65 वर्ष।
14. भारत में किसे अभिलेख न्यायालय माना गया है?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय को।
15. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है?
उत्तर:
संसद के पास।
16. न्यायायिक सक्रियता की आवश्यकता के दो कारण लिखें।
उत्तर:
सरकार की कमजोरी एवं देश में फैला व्यापक भ्रष्टाचार ।
रिक्त स्थान भरें
1. “सर्वोच्च न्यायालय ने समस्त संघात्मक ढाँचे को संबद्ध रखने में सीमेंट का काम किया है।” यह कथन का है।
उत्तर:
हरमन फ़ाइनर
2. सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद …………….. में की गई है।
उत्तर:
124
3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ………….. को हुआ।
उत्तर:
28 जनवरी, 1950
4. सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ……………. को सलाह दी जाती है।
उत्तर:
राष्ट्रपति
5. पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय ……………. में स्थित है।
उत्तर:
चण्डीगढ़
6. संघीय व्यवस्था का संरक्षक ………….. होता है।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय
7. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर …………… वर्ष तक रह सकते हैं।
उत्तर:
65
8. मौलिक अधिकारों की रक्षा ………………. के द्वारा की जाती है।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय
9. भारत में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ………………. प्रणाली द्वारा की जाती है।
उत्तर:
कॉलेजियम
10. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ………………. द्वारा की जाती है।
उत्तर:
मुख्य न्यायाधीश
11. भारत में इस समय कुल ………………. उच्च न्यायालय हैं।
उत्तर:
25
12. ………………. भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालय
![]()
![]()
![]()
![]()