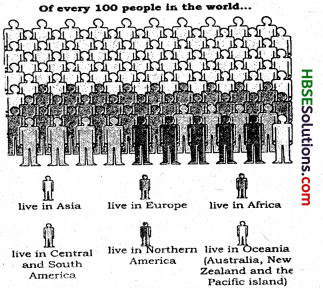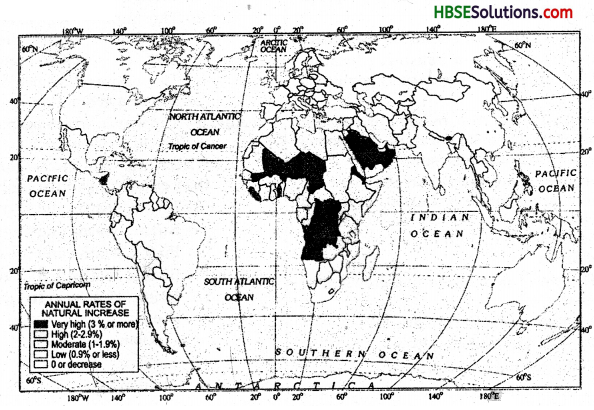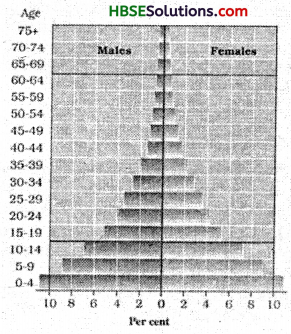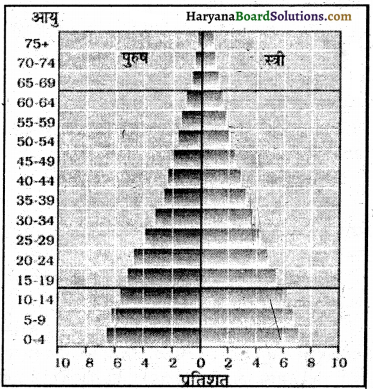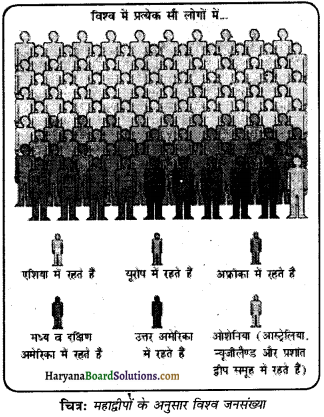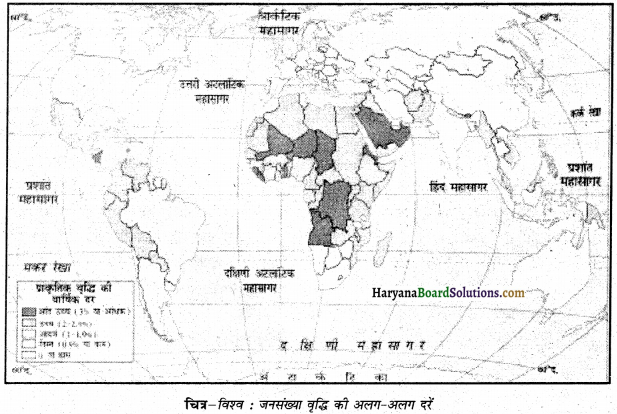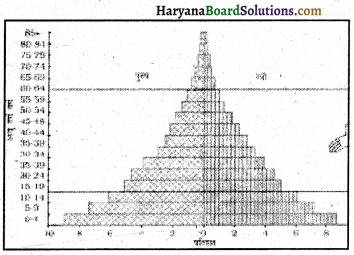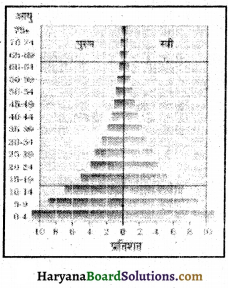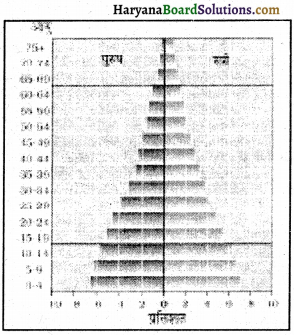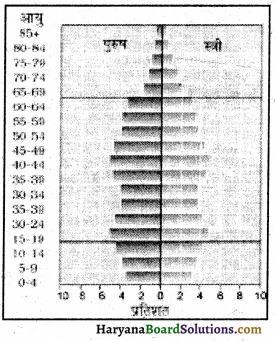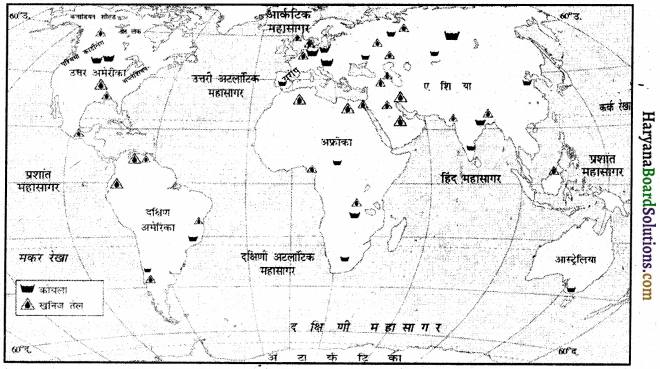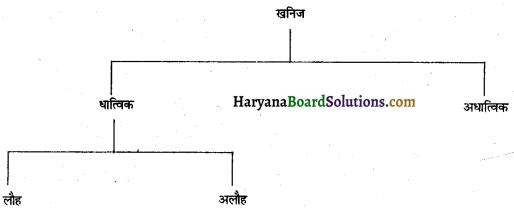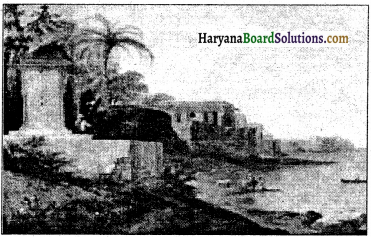Haryana State Board HBSE 8th Class Social Science Solutions History Chapter 5 जब जनता बगावत करती है (1857 और उसके बाद) Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 8th Class Social Science Solutions History Chapter 5 जब जनता बगावत करती है (1857 और उसके बाद)
HBSE 8th Class History जब जनता बगावत करती है (1857 और उसके बाद) Textbook Questions and Answers
फिर से याद करें
जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद Notes HBSE 8th Class प्रश्न 1.
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या माँग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया?
उत्तर:
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से माँग थी कि उसने अपने पति के देहांत के बाद जिस बच्चे को गोद में लिया था उसे वे झाँसी की गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दें। उसने झाँसी राज्य (जो उस समय एक स्वतंत्र राज्य था) की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा झाँसी के राज्य परिवार के हितों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की जिसे उसने ठुकरा दिया।
जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद प्रश्न उत्तर HBSE 8th Class प्रश्न 2.
ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया?
अथवा
भारत में नए ईसाइयों के हितों में अंग्रेजों ने जो कदम उठाए, उनके भारतीयों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े?
उत्तर:
I. उपाय तथा कानून (Measures and Laws) :
(i) 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी।
(ii) 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा।
II. प्रभाव (Effect) : बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति-रिवाज और परंपरागत जीवनशैली को नष्ट कर रहे हैं।

जब जनता बगावत करती है HBSE 8th Class History प्रश्न 3.
सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था?
उत्तर:
एन्फील्ड नामक राइफलों के प्रयोग ने विद्रोह आरंभ करने वाली चिंगारी का काम किया। इन राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बियों का प्रयोग होता था। यह बात हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के लिए समान रूप से आपत्तिजनक थी। सर्वाधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि सैनिकों को बंदूक में कारतूस भरने से पहले इन्हें मुँह से काटना पड़ता था। जंगल में लगी आग की तरह यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू तथा मुसलमान सैनिक भड़क उठे। सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजों ने जान-बूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने के लिए ही कारतूसों में चर्बी का प्रयोग किया है।
जब जनता बगावत करती है 1857 उसके बाद HBSE 8th Class History प्रश्न 4.
अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए?
उत्तर:
सितंबर, 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह को अक्तूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र ने अंतिम सांस ली। उसके अंतिम शब्द ये थे-“इतना है बदनसीब जफ़र, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में।” आज भी हम उस बदनसीब बादशाह की मजार रंगन में देख सकते हैं। बहादुरशाह जफ़र स्वतंत्रता की लड़ाई में एक कमजोर कड़ी साबित हुआ। उसमें नेतृत्व करने की शक्ति का अभाव था। फिर भी 1857 की क्रांति में उसका नेतृत्व महत्त्वपूर्ण रहा।
आइए विचार करें
जब जनता बगावत करती है प्रश्न उत्तर HBSE 8th Class History प्रश्न 5.
मई, 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे?
उत्तर:
निम्नलिखित कारणों से मई 10, 1857 से पूर्व भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों में आत्मविश्वास था:
1. 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान, दोनों खत्म होते जा रहे थे।
2. बहुत सारे देशी राज्यों के दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। वे कंपनी की इच्छानुसार सैनिक प्रशासन को चलाते थे।
3. स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था।
4. उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक-एक करके छीने जा रहे थे।
5. बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थीं कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले।
6. मुगलों के बाद कुछ समय के लिए मराठा बहुत शक्तिशाली रहे थे। लेकिन बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया।
उपरोक्त घटनाओं के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस समय तक अंग्रेजों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था।
प्रश्न 6.
बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज-परिवारों पर क्या असर पड़ा?
उत्तर:
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा 1857 के विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए विवश किया गया। उनके द्वारा उन्हें समर्थन देने से देश की जनता और अन्य राज-परिवारों पर निम्न प्रभाव पड़े :
1. मेरठ से चलकर दिल्ली पहुँचने वाले विद्रोही सिपाही लाल किले की दीवारों के आस-पास जमा हो गए। वे मुगल बादशाह बहादुर शाह से मिलना चाहते थे। वृद्ध बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो-दो हाथ करने को तैयार नहीं था लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नेता घोषित कर दिया।
2. बूढे बादशाह को सिपाहियों की यह माँग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं (Chiefs) और शासकों (Rulers) को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ (Union) बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुरशाह ज़फ़र का नेतृत्व इस मोड़ पर आकर बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया।
3. अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र (without any worry) होकर चलाने लगेंगे।
4. अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह ज़फ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातोरात बदल गई। सर्वत्र विद्रोह फैलता चला गया। प्रायः ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है।
5. जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। जैसे-जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा।
6. झाँसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मेलीं। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बहादुरशाह जाफर के तृत्व ने देश में एक अच्छा संदेश दिया।

प्रश्न 7.
अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया?
उत्तर:
1. अवध के बागी भू-स्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने कई कार्य किए। उन्होंने उन्हें अपनी निजी सेनाएँ भंग करने के लिए विवश किया। उन्हें कहा गया कि विद्रोह के बाद जिन जमींदारों के विरुद्ध गंभीर हिंसात्मक आरोप नहीं होंगे उन्हें उनके भ-भाग वापस कर दिए जायेंगे क्योंकि अवध की राजधानी लखनऊ में क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक था। यहाँ क्रांति का नेतत्व बेगम हजरत महल ने किया था। महारानी ने अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया।
2. अंग्रेजों की चालों का जमींदारों पर प्रभाव नहीं देखा गया। समस्त प्रदेश के जमींदारों तथा ताल्लुकदारों ने क्रांति में भाग लिया और जहाँ भी अंग्रेज मिले उनका वध कर दिया गया और उनके भवनों को जलाकर राख कर दिया। सारा अवध अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया।
3. जनरल हैवलॉक एक विशाल सेना लेकर कानपुर से लखनऊ गया जहाँ क्रांतिकारियों ने उसको परास्त कर दिया। वह रेजीडेंसी की ओर गया, किंतु वहाँ भी क्रांतिकारियों ने उसको परास्त कर दिया।
4. अंग्रेजों के सौभाग्य से इसी समय गोरखों की सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए आ गई। गोरखों की सहायता से अंग्रेजों का लखनऊ पर अधिकार हो गया। भीषण युद्ध के बाद अंग्रेज विजयी हुए। इसके बाद नील और कैंपबैल सेनाएँ लेकर अवध के भू-स्वामियों को कुचलने के लिए निकल पड़े।
प्रश्न 8.
1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदलीं?
उत्तर:
अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे:
1. कंपनी के शासन का अंत (End of the rule of the Company): ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को अब ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके।
2. भारतीय सरकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा ताज के अधीन (Indian Government under direct control of the British Cabinet and the Crows) : ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर-जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा/रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अन्य शब्दों में ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली।
3. भारतीय शासकों के प्रति नीति में बदलाव (Changes in policies towards the Indian Princes or rulers) : देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई।
4. सेना में परिवर्तन (Changes in Army) : सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे।
5. मुसलमानों के प्रति शत्रुता की नीति (Policy of enmity towards Muslims) : मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था।
6. धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) : 1858 ई. की महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिलाया गया। भारतीयों को धार्मिक कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
7. वित्त व्यवस्था का पुनर्गठन (Reorganization of Financial System): 1857-58 ई. के विद्रोह के दौरान भारत सरकार का इतना धन खर्च हो गया था कि उस पर लगभग । करोड़ पौंड का ऋण चढ़ गया था। इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए वित्त व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया और धन एकत्र करने के लिए भूमि कर, आय कर और लाइसेंस कर आदि की दरें बढ़ा दी गई। सरकार के प्रत्येक विभाग में बचत करने की कोशिश की गई। मुक्त व्यापार प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार चाय, पटसन आदि को बिना कर के दूसरे देशों में भेजा जाने लगा तथा भारत के आयात पर भी कर कम कर दिए गए।
8. भारतीयों के लिए कल्याण कार्य (Welfare works -for the Indians) : यह घोषणा की गई कि भविष्य में सरकार भारतीयों के कल्याण तथा औद्योगिक और बौद्धिक विकास के लिए कार्य करेगी। नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर होंगी और भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
9. इंडियन कौंसिल्ज एक्ट, 1861 ई. (Indian Council Act, 1861) : सर सैय्यद अहमद खां और सर बार्टल फ्रायर ने विचार व्यक्त किया था कि विद्रोह का एक कारण शासन में भारतीयों की भागीदारी न होना भी था। इसलिए 1861 ई. में इंडियन कौंसिल्ज एक्ट पारित किया गया जिसके अनुसार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में स्थान दिया गया और प्रांतों में भी विधान परिषदें स्थापित की गई। संवैधानिक दृष्टिकोण से यह विद्रोह का महत्त्वपूर्ण परिणाम था।
10. भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध (Restrictions on Indian Newspapers): 1857 ई. के विद्रोह के बाद सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए और उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। सरकार को डर था कि यह समाचार पत्र कहीं विद्रोही भावनाओं को न भड़का दें।

आइए करके देखें
प्रश्न 9.
पता लगाएँ कि सन सत्तावन की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं? इस महान विद्रोह से संबंधित कौन-सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं?
उत्तर:
विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं।
उपयोगी संकेत (Useful Hint)
1. गीत : बुंदेले हर बोलो से……
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसीवाली रानी थी। नामक गीत पढ़ें तथा याद करके लिखें।
2. उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) की राजधानी लखनऊ में रेजिडेंसी के निम्न खंडहर से संबंधित एक छोटी कहानी नीचे दी गई है:
जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतों, मदों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोलों से हमला किया। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं।
प्रश्न 10.
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएँ। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं?
उत्तर:
झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई :
1. 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक भारतीय नर-नारियों ने अपने जीवन की आहुति दी परंतु झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का त्याग, अपूर्व साहस तथा अद्भुत वीरता भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी।
2. लार्ड डलहौजी की विलय की नीति के कारण रानी अंग्रेजों के विरुद्ध थी। झाँसी के राजा गंगाधर राव की अचानक मृत्यु हो गई तथा रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को कंपनी ने उसके उत्तराधिकारी के रूप से मान्यता नहीं दी। झाँसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाकर रानी की 60,000 रु. वार्षिक पेंशन नियत कर दी गई परंतु रानी ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने झाँसी की सेनाओं को तोड़ दिया। मेजर अरिस्कन (Major Eriskin) को झाँसी का ब्रिटिश रेजीडेंट नियुक्त किया गया।
3. झाँसी की रानी अंग्रेजों की विलय नीति का शिकार हुई थी। 1857 के विप्लव में वह कूद पड़ी। उसने सेना का संगठन करके अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उसका दमन करने के लिए मार्च 1858 ई. में सर यूरोज झाँसी की ओर चला। रानी ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उसने अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिए। रानी के निमंत्रण पर तात्या टोपे अपनी सेना लेकर उसकी सहायता के लिए चल पड़ा, किंतु मार्ग में ही सर यूरोज ने उसे परास्त कर दिया।
4. झाँसी की दशा भी चिंताजनक हो गई। अंग्रेजों के लगातार हमले हो रहे थे किंतु वे झाँसी पर अधिकार करने में असफल रहे। अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल चली और कुछ सैनिकों को अपनी ओर तोड़ लिया। इन सैनिकों ने दक्षिण द्वार खोल दिया। अंग्रेजी सेना उस द्वार से झाँसी में घुस गई।
5. शीघ्र ही दूसरा द्वार भी टूट गया और उस द्वार से भी अंग्रेज सेना अंदर आ गई। रानी ने अपने बच्चे को कमर से बाँधा और अंग्रेजी सेना को चीरती हई झाँसी से बाहर निकल गई और तात्या टोपे के पास कालपी पहुँची। सर यूरोज ने उसका पीछा किया। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसको अपने अधिकार में कर लिया। सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया। पहले वह परास्त हुआ किंतु उसने बाद में रानी की सेना को घेर लिया।
6. रानी ने भागना उचित समझा। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया। अचानक उसका घोड़ा एक नाले में गिर गया। अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण कर उसको घायल कर दिया। वह इस अवस्था में भी अंग्रेजों से लड़ती रही किंतु कुछ समय पश्चात् 17 जून 1858 ई. को उसकी मृत्यु हो गई।
उस समय अंग्रेजों की शक्ति से लोहा लेना एक महिला की विलक्षणता को सिद्ध करता है।
आइए कल्पना करें
कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं। विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे?
उत्तर:
1. मैं चपाती या कमल शब्द एक गुप्त शब्द (code word) के रूप में प्रयोग करता। मैं अपनी भावी योजनाओं को अपने परिवारजनों से भी गुप्त रखता। विद्रोह के दौरान कमल या चपाती शब्द का ही प्रयोग देश-भक्तों के द्वारा गुप्त समितियों में किया जाता था।
2. मैं उसी क्षेत्र की वेशभूषा धारण करता जहाँ मैं अपनी गुप्त समितियों से रात्रि के वक्त बातचीत करता। मैं एक समूह मुस्लिम सिपाहियों का तथा दूसरा हिंदू सिपाहियों का बनाता। उन्हें उनके धार्मिक ग्रंथों-पवित्र कुरान तथा पवित्र भगवतगीता पर देश के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाता। हम गुप्त सभायें कभी मंदिर तो कभी मस्जिदों में रखते। चकमा देने के लिए कभी-कभी ग्रामीण मेलों का भी प्रयोग किया जाता।
3. हम विद्रोह की सफलता के लिए अपने नेता बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकालकर कहीं और ले जाते ताकि वह अंग्रेजों के हाथों में न आते। हम सभी साथी हर तरह की नीतियाँ-साम, दाम, दंड, भेद अपनाकर ब्रिटिश अधिकारियों को तोड़ने की कोशिश करते। युद्ध एवं प्यार में जब हर चीज अंग्रेज उचित मानते थे तो हम आदर्शों की पिटारी क्यों पीटते। अंग्रेजों को धोखा देने में हम कभी भी नहीं हिचकिचाते।
HBSE 8th Class History जब जनता बगावत करती है (1857 और उसके बाद) Important Questions and Answers
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
रेजिडेंटस कौन था?
उत्तर:
जो भारतीय राज्य (रियासतें) सहायक संधि की शर्ते मानकर उस पर हस्ताक्षर करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन राज्यों में अपना एक प्रतिनिधि भी नियुक्त करती थी जिसे रेजीडेंट कहते थे। वह उस राजा के दरबार में रहकर वास्तव में उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखता था।
प्रश्न 2.
भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध महान विप्लव (बगावत/विद्रोह) कब तथा कहाँ शुरू हुआ था?
उत्तर:
10 मई, 1857 को मेरठ में।
प्रश्न 3.
मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने किसे विद्रोह का नेता तथा संपूर्ण भारत का सम्राट घोषित किया था?
उत्तर:
80 वर्षीय वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को जो विद्रोह के उपरांत देश में अंतिम मुगल सम्राट साबित हुआ था।

प्रश्न 4.
वेल्लोर में कंपनी के सिपाहियों में किसने विद्रोह को भड़काया था?
उत्तर:
मैसूर के टीपू सुल्तान के पुत्रों ने।
प्रश्न 5.
बिहार में विद्रोही शक्तियों का नेता कौन था?
उत्तर:
कुंवर सिंह (Kunwar Singh)।
प्रश्न 6.
महान विद्रोह के दौरान कौन एकता के प्रतीक के रूप में उभरा था?
उत्तर:
बहादुरशाह ज़फ़र।
प्रश्न 7.
कब और कैसे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी?
उत्तर:
वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती हुई जून 1858 में शहादत (मृत्यु) को प्राप्त हुई।
प्रश्न 8.
सिपाहियों, शासकों एवं मुखियाओं का समान लक्ष्य क्या था जिसके कारण उन्होंने 1857 के विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया था?
उत्तर:
भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा मुगल सम्राट के नेतृत्व में अपनी सरकार स्थापित करना।
प्रश्न 9.
नाना साहेब कौन था?
उत्तर:
पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र।
प्रश्न 10.
बख्त खान कौन था?
उत्तर:
दिल्ली में भारतीय सैनिकों को 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक कमांडर-इन-चीफ के रूप में उन्होंने (बख्त खान ने) नेतृत्व प्रदान किया था।
प्रश्न 11.
विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था?
उत्तर:
बहादुर शाह ज़फ़र को।
प्रश्न 12.
वे कौन-कौन से क्षेत्र थे जहाँ विप्लव सर्वाधिक विस्तृत रहा था?
उत्तर:
देहली, अवध (लखनऊ), रुहेलखंड, बुंदेलखंड (झाँसी), इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, आगरा, मेरठ एवं पश्चिमी बिहार।

प्रश्न 13.
भारतीय इतिहास में 1857 के वर्ष का क्या महत्त्व है?
उत्तर:
1857 का वर्ष भारत के इतिहास में इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार अनेक कारणों से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एक साथ बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय किया तथा एक लंबा संघर्ष किया।
प्रश्न 14.
मंगल पांडे कौन था?
उत्तर:
मंगल पांडे बैरकपुर स्थित अंग्रेजी सैन्य शिविर में एक साहसी तथा वीर सैनिक था। वह पहला वीर सैनिक था जिसने एनफील्ड नामक नयी राइफल में चर्बी वाले कारतूसों को भरने से इंकार कर दिया था। इसी कारण उसे गिरफ्तार किया गया तथा बाद में उसे फांसी की सजा दे दी गई।
प्रश्न 15.
उन प्रमुख भारतीय नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
उत्तर:
1857 के विद्रोह में जिन प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, वे थे:
- मंगल पांडे
- मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र
- नाना साहेब
- बखत खान
- कुवर सिंह
- तात्या टोपे तथा
- लक्ष्मीबाई।
प्रश्न 16.
1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। .
उत्तर:
1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे : बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, झाँसी (बुंदेलखंड), हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ।
प्रश्न 17.
1857 के विद्रोह का अधिकांश स्थानों पर किसने नेतृत्व किया था? उनकी मौलिक दुर्बलता क्या थी?
उत्तर:
अधिकांश स्थानों पर 1857 की बगावत का नेतृत्व देशी नरेशों (शहजादों) तथा भू-स्वामियों के हाथों में ही था। (यद्यपि इसे भारतीय कंपनी के सिपाहियों ने प्रारंभ किया था।) भारतीय शासकों एवं भू-स्वामियों की मुख्य दुर्बलता यह थी कि उनके विचार पुराने थे तथा मूलतः वे अपने या अपने परिजनों के स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही लड़े थे।
प्रश्न 18.
1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को कैसे प्रभावित किया था?
उत्तर:
1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। एक नये अधिनियम के अनुसार उससे सत्ता छीन कर ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सौंप दी गई। वह भारत सचिव के नेतृत्व में ब्रिटेन के साम्रज्ञी के नाम से शासन करने लगा।
प्रश्न 19.
किस गवर्नर-जनरल के काल में 1857 की बगावत शुरू हुई थी?
उत्तर:
लार्ड कैनिंग।
प्रश्न 20.
जब 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, उस | समय मुगल सम्राट (शासक) कौन था?
उत्तर:
बहादुर शाह जफ़र।
प्रश्न 21.
अंग्रेजों के विरुद्ध वेल्लोर में विद्रोह कब हुआ
उत्तर:
1806 में।
प्रश्न 22.
1857 के विद्रोह (बगावत) को अन्य क्या महत्त्वपूर्ण एवं आकर्षक नाम (संज्ञा) दिया जाता है?
उत्तर:
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम।
प्रश्न 23.
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था।
उत्तर:
नाना साहेब।

प्रश्न 24.
1857 के विद्रोह की असफलता का सर्वाधिक जिम्मेदार कारण क्या था?
उत्तर:
भारतीय शासकों में पूर्ण एकता का अभाव तथा परस्पर ईर्ष्या या द्वेष।
प्रश्न 25.
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था?
उत्तर:
चर्बी वाले कारतूस, जिन्हें मुंह से खोलकर (काटकर) एनफील्ड राइफल में भरा जाता था। चर्बी (अफवाहों के अनुसार) गाय तथा सूअर की थी।
प्रश्न 26.
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नाना साहेब का मुख्य परामर्शदाता, 1857 के विद्रोह के वक्त कौन था?
उत्तर:
अजीमुल्लाह।
प्रश्न 27.
नाना साहेब की सेनाओं को 1857 में किसने नेतृत्व दिया था?
उत्तर:
तात्या टोपे।
प्रश्न 28.
झाँसी में 1857 के विद्रोह में विद्रोही सेनाओं को किसने नेतृत्व दिया था?
उत्तर:
रानी लक्ष्मीबाई।
प्रश्न 29.
उन कुछ नेताओं या नायकों के नाम लिखिए जिनकी गतिविधियाँ 1857 के विद्रोह के दौरान कालांतर में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गयी थीं।
उत्तर:
मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बख्त खान, जीनत महल, कुंवर सिंह, नाना साहेय। .
प्रश्न 30.
रंगून किस देश की राजधानी है?
उत्तर:
बर्मा (आजकल इसे म्यांमार कहते हैं।)।
प्रश्न 31.
निम्नलिखित शब्दों/पदों के अर्थों की व्याख्या कीजिए:
(i) सैनिक विद्रोह (बगावत) (Mutiny), (ii) फिरंगी (Firangis)।
उत्तर:
- सैनिक विद्रोह (Mutiny): जब सिपाही एकत्र होकर अपने सैनिक अफसरों का कोई भी आदेश मानने से इंकार कर देते हैं।
- फिरंगी (Firangis) : विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव हुपा है और विदेशी शासनकाल के दौरान यह उपनिवेशवादी शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था।
लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
मेरठ में महान विद्रोह अथवा विप्लव के प्रारंभ होने की घटना पर चर्चा कीजिए।
उत्तर:
मेरठ में विद्रोह (बगावत) का प्रारंभ :
1. 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फाँसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फोजी अभ्यास करने से इंकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का आदेश न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है।
2. मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे।
प्रश्न 2.
मेरठ से दिल्ली तक 1857 के विद्रोह की अग्नि । कैसे फैली? दिल्ली से संबंधित कुछ घटनाओं का ब्यौरा दीजिए।
उत्तर:
1. मेरठ के विद्रोही सिपाहियों के सामने प्रश्न यह आ गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन, चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूँढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे।
2. मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह-अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए।
3. देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला-बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो-दो हाथ करने को तैयार नहीं थे लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया।

प्रश्न 3.
अंग्रेजों द्वारा जो सामाजिक सुधार शुरू किए गए थे उनका भारतीय समाज के एक हिस्से द्वारा क्यों विरोध किया गया था?
उत्तर:
ब्रिटिश सामाजिक सुधारों पर भारतीय समाज के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया :
1. सती प्रथा का अंत (End of Sat) : लार्ड विलियम बैंटिंक ने सती प्रथा पर कानून द्वारा रोक लगा दी थी तथा इसे आत्महत्या के बराबर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया था। इस कार्य को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति को हत्या के समान अपराध का दंड दिया जाना निश्चित हुआ। विधवाओं को पुनः विवाह की आज्ञा मिल गई। कट्टरपंथी हिंदू लोगों ने गवर्नर-जनरल के इस कार्य को अपने धर्म में एक अनुचित दखल माना। वे क्रुद्ध हो उठे तथा अंग्रेजी शासन को उलट देने का अवसर आते ही उसको सहयोग देने को तैयार हो गए।
2. विदेशी शिक्षा पद्धति एवं भाषा को थोपना (Impart of foreign educational system and language): अंग्रेजों ने भारत की परंपरावादी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर अपने ढंग की शिक्षा-पद्धति और अंग्रेजी भाषा को भारतीयों पर थोप दिया। आम जनता इससे क्षुब्ध हो उठी तथा अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के लिए बलिदान देने को तैयार हो गई।
3. सामाजिक आचारों में हस्तक्षेप (Intervene in Social Culture): अंग्रेजों ने भारतीय समाज में व्याप्त बाल विवाह को बंद कर दिया तथा विधवा विवाह की आज्ञा दे दी। मानव बलि तथा कन्यावध को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। रूढ़िवादी हिंदुओं ने इन सब बातों को अपने धर्म के विरुद्ध समझा।
4.ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ (Activities of the Christian Misionaries) : धर्म प्रचारकों ने अनेक स्थानों पर लोगों की दरिद्रता, सामाजिक पिछड़ापन तथा जाति प्रथा की कुरीतियों का लाभ उठाकर उन्हें ईसाई धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित किया। अनेक स्कूलों, बाजारों, अस्पतालों एवं जेलों में ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें धन तथा अन्य रूपों में सहायता दी। नव ईसाइयों को आसानी से सरकारी नौकरियां मिल जाती थीं। लोगों के धर्म परिवर्तन से रूढ़िवादी हिंदू एवं मुसलमान अंग्रेजों के शत्रु बन गए।
5. पैतृक संपत्ति के नियमों में परिवर्तन (Changes in the laws of parentel property) : लार्ड डलहौजी ने एक कानून बनाकर यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति धर्म बदलेगा उसे धर्म परिवर्तन के कारण पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इससे लोगों में धार्मिक असुरक्षा की भावना बढ़ी।
प्रश्न 4.
भारतीय राज्यों के अंग्रेजों द्वारा विलीनीकरण का आम लोगों के आर्थिक जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा था?
उत्तर:
अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों के विलीनीकरण का साधारण लोगों के आर्थिक जीवन पर पड़े प्रभाव (The economic effects on the life of the common people due to annexation of the Indian states by the British):
1. भारतीय साधनों का शोषण करके देश को निर्धन बनाया : यद्यपि इससे पहले भी भारत ने अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे थे किंतु किसी का उसके आर्थिक ढाँचे पर इतना गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ विदेशी लुटेरों को छोड़कर दिल्ली के सिंहासन पर जो भी वंश आया, उसने भारत के धन को इसकी सीमाओं से बाहर ले जाने का प्रयास नहीं किया। फलत: भारत का धन भारत में ही रहा परंतु अंग्रेजों के काल में कंपनी की आर्थिक नीति लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित होती थी।
इस प्रकार भारत का धन तथा साधन इंग्लैंड के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ भेजे जाने लगा। भारत के आर्थिक साधनों का शोषण होने लगा जिसके कारण परंपरागत भारतीय उद्योग नष्ट हो गए और भारत निर्धन व बेरोजगारों का देश बन गया। किसानों का शोषण बढ़ा। कृषि गतिहीन हो गई। लाखों लोग बार-बार पड़ने वाले अकालों के शिकार बने।
2. राज्यों में नौकरियों तथा पदोन्नति आदि पर प्रभाव : भारतीय राज्यों के कंपनी में विलीनीकरण से प्रत्येक राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी का उन्मूलन कर दिया गया। फलस्वरूप -अनेक भारतीय बेरोजगार हो गए। जो लोग भारतीय राज्यों में इतिहासकारों, कलाकारों आदि के रूप में देशी राजाओं द्वारा संरक्षण, अनुदान राशि आदि पाये हुए थे, एक तरह से आर्थिक रूप से उन पर अवलंबी थे, वे भी बेरोजगार और बेसहारा हो गए। स्वयं कंपनी ने सेना, प्रशासन आदि से संबंधित ऊँचे पदों पर भारतीयों के लिए अवसर बहुत ही सीमित कर दिए गए थे। इससे समाज के उच्च वर्गों में भी बेरोजगारी फैल गयी।
3. अनेक राज्यों में बड़ी-बड़ी पैदल सेनाएँ, हाथी सवार, घोड़े सवार, नावों पर माल लाने ले जाने वाले रक्षक आदि भी राज्यों के विलीनीकरण के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गए। इस संदर्भ में अवध राज्य का एक अच्छा उदाहरण है। सहायक संधि के कारण भी अनेक देशी राज्यों की सेनाओं को तोड़ दिया गया था।
4. अनेक शिल्पकार जो राज्यों के संरक्षण पर निर्भर थे, वे भी बेरोजगार हो गए।
प्रश्न 5.
क्या 1857 का विद्रोह एक लोकप्रिय चरित्र वाला विद्रोह था? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।
अथवा
अपने तर्क देकर बताइए कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
उत्तर:
अनेक भारतीय विद्वानों तथा इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भारतीय जनता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। यह एक लोकप्रिय विद्रोह था। इसमें सैनिकों, भारतीय नरेशों, जमींदारों के साथ-साथ सर्वसाधारण वर्ग के किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों ने भी भाग लिया था। यह व्यापक जनसमर्थन लिए हुए था। इस मत के प्रवर्तक विनायक दामोदर और वीर सावरकर हैं। उन्होंने सर्वप्रथम 1909 ई. में अपनी ‘भारत की स्वतंत्रता का युद्ध’ नामक पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत के लोगों का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा है।
उनके विचारों का समर्थन एस. पांडिकर, अशोक मेहता, जे. सी. विद्यालंकार तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है। इसे उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इन विद्वानों के अनुसार इस विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर कर एक राष्ट्रीय शासक को सत्ता सौंपना था। इसका क्षेत्र व्यापक था। यह विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों के कारण काफी जल्दी फैला तथा इसमें सैनिकों, जमींदारों, राजाओं के साथ-साथ साधारण वर्ग के अनेक लोगों ने भाग लिया।

प्रश्न 6.
1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश सेना में क्या-क्या सुधार किए गए थे?
उत्तर:
1857 के बाद ब्रिटिश सेना में निम्नलिखित सुधार (या परिवर्तन) किए गए थे :
1. अंग्रेजों ने सबसे पहली जिस बात को अपने मस्तिष्क में रखा वह यह थी कि सेना पर अंग्रेज सैनिक अधिकारियों एवं सिपाहियों का ही यथासंभव वर्चस्व सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में अब यह | अनुपात एक और दो का तथा मद्रास और बंबई की सेनाओं में दो और पाँच का था।
2. सभी भौगोलिक और सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर यूरोपीय सैनिकों को ही नियुक्त किया गया। तोपखाने (और बाद में 20वीं शताब्दी में). टैंकों तथा बख्तरबंद गाड़ियों के महत्त्वपूर्ण विभाग पूर्णतया यूरोपियों विशेषकर अंग्रेजों के हाथों में ही रखे गए।
3. अधिकारी वर्ग में भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का सख्ती से पालन किया जाने लगा। 1914 ई. तक कोई भी भारतीय सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठ सका।
4. सेना में भारतीय अंग का संगठन “संतुलन एवं जवाबी संतुलन” तथा “बाँटो और शासन करो” (Divide and Rule) की नीति के आधार पर किया गया ताकि किसी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह | के लिए एकजुट होने का उनको मौका ही न मिल सके।
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
वेल्लौर में विद्रोह (बगावत) क्यों हुई थी? इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था?
उत्तर:
1806 में हुए वेल्लौर विद्रोह के कारण (Causes of the Vellore Mutiny of 1806):
1. अनेक विद्वान मानते हैं कि 1857 के प्रथम लोकप्रिय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि के रूप में दक्षिण भारत में 1806 में ही वेल्लौर का विद्रोह हो चुका था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा इतिहासकार वीर सावरकर के विचारानुसार वेल्लौर के विद्रोह ने ही वस्तुतः 1857 के विद्रोह की नींव रखी थी।
2. 1799 में मैसूर के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान टीपू सुल्तान को उसकी राजधानी श्रीरंगपटनम के पास हुई एक लड़ाई में पराजित किया गया था और उसे गोली मार दी गयी थी। इससे मैसूर की जनता तथा टीपू के वफादार बहुत ही अंग्रेजों से नाराज थे।।
3. टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने शाही परिवार पर अत्याचार शुरू किए। टीपू के सभी 12 पुत्रों एवं 6 लड़कियों को वेल्लौर के किले में कैद कर लिया गया।
4. टीपू के अनेक सैनिकों तथा सामंतों की भंग की गयी सेनाओं को अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती कर उनकी वफादारी खरीदने तथा सेना में भी ‘फूट डालो तथा राज करो’ की नीति लागू कर दी। जो ब्रिटिश प्रभाव से बाहर थे उन्होंने भी वेल्लौर विद्रोह में भाग लेने का निर्णय ले लिया था।
5. टीपू के उत्तराधिकारियों एवं अनेक वफादार सिपाहियों ने संगठित होकर पुनः शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया।
6. अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कई सैनिक परिवर्तन किए थे। उन्हें आज्ञा दी गई कि वे अपनी पुरानी बड़ी-बड़ी दाढ़ी तथा मूंछे मुंडवा दें जिन्हें पुराने सैनिक पसंद नहीं कर रहे थे। .
7. एक अंगन्यू (Angnew) नामक अंग्रेज सैन्य ऑफिसर ने भारतीय सैनिकों के लिए एक नई किस्म की पगड़ी पहनना अनिवार्य कर या जिसे सैनिकों ने पसंद नहीं किया। इस पगड़ी पर एक क्रॉस (Uross) का चिह्न लगाना अनिवार्य कर दिया गया जिसम विरोध हिंदू तथा मुस्लिम सिपाहियों ने किया था। इस नयी पगड़ी पर एक नयी मुर्गे की तरह कलगी (cockade) या पंख लगाया जाता था जो संदेह किया गया कि वह सूअर तथा गाय के चमड़े से बना होता था।
प्रश्न 2.
1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा | कीजिए।
अथवा
1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित क्रांतिकारियों/ विद्रोहियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
(i) बैरकपुर में मंडल पांडे।
(ii) मेरठ में भारतीय सिपाही।
(iii) विद्रोही तथा बहादुरशाह जफर दिल्ली में।
(iv) कानपुर में नाना साहेब।
(v) लखनऊ एवं प्रमुख विद्रोही।
(vi) झाँसी में रानी लक्ष्मीबाई।
(vii) मध्य भारत में तात्या टोपे।
उत्तर:
1857 के महान विद्रोह (बगावत) विप्लव की प्रमुख घटनाएँ:
(i) बैरकपुर में मंगल पांडे (Mangal Pandey at Barackpur) : सर्वप्रथम बैरकपुर में विद्रोह का आरंभ हुआ जब 23 जनवरी, 1857 ई. को दमदम के सभी सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से इंकार कर दिया। 29 मार्च, 1857 ई. को मंगल पांडे ने अपने साथियों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। मंगल पांडे को साजेंट ह्यूसन और लैफ्टिनेंट बाग ने पकड़ने की कोशिश की परंतु उसने दोनों अफसरों को गोली से उड़ा दिया। फिर अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी आई। मंगल पांडे को पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल, 1857 ई. को उसे फांसी दे दी गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वह प्रथम शहीद था। विद्रोहियों ने क्रांति के लिए 31 मई का दिन निश्चित किया था परंतु परिस्थितियों के कारण यह आग पहले ही भड़क उठी। बंगाल से यह आग मेरठ पहुंची।
2. मेरठ में भारतीय सिपाही (Indian Sepoys at Meerut) : 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। उम पर मुकदमा चलाया गया और 9 मई, 1857 ई. को 85 सैनिकों को जेल भेज दिया गया। 10 मई को मेरठ के अन्य भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वे ‘हर हर महादेव’ और ‘मारो फिरंगी’ के नारे लगाने लगे। तत्पश्चात् उन्होंने स्थानीय जेल को तोड़ अपने साथियों को रिहा कराया और फिर नगर में रहने वाले अंग्रेज नर-नारियों का वध कर दिया। अगले दिन वे बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर चल पड़े।
3. दिल्ली में विद्रोही तथा बहादुरशाह जफर (Rebels at Delhi and Bahadur Shah Zafar): मई के प्रात:काल मेरठ से सैनिक दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने दिल्ली के सैनिकों को साथ देने के लिए ललकारा। यहाँ के सैनिकों में पहले ही विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। वे शीघ्र ही उनमें सम्मिलित हो गए और जो भी अंग्रेज उनके सामने आया उनका वध कर डाला गया। इन सैनिकों का बारुदखाने पर अधिकार होने से पहले ही अंग्रेज अफसरों ने उनमें आग लगा दी। अब सैनिकों ने लाल किले में प्रवेश किया और बहादुरशाह को सम्राट घोषित किया। नगर में सम्राट का जुलूस निकाला गया।
इस प्रकार दिल्ली पर सैनिकों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। शीघ्र ही यह समाचार दिल्ली के निकट प्रदेशों में फैल गया कि क्रांतिकारियों ने दिल्ली को स्वतंत्र करा लिया है। प्रोत्साहित होकर इन क्षेत्रों में क्रांति फैल गई। अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी तथा रूहेलखंड (मुरादाबाद व बरेली) में भी अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा सरकारी कोष पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। इस प्रकार शीघ्र ही दिल्ली और उसके निकट के समस्त प्रदेशों पर मुगल सम्राट बहादुरशाह का झंडा फहराने लगा और – वहाँ के अंग्रेजी राज्य का अंत हो गया। साधारण जनता ने सैनिकों का स्वागत किया तथा उन्हें सब प्रकार की सहायता प्रदान की।
4. कानपुर में नाना साहेब (Nana Saheb at Kanpur) कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया। उसके सैनिकों ने नगर के दुर्ग पर आक्रमण किया और अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने लगभग 200 अंग्रेजों का वध कर दिया। अंत में जनरल हैवलाक, जनरल नील, जनरल कैंपबेल आदि ने विद्रोहियों की शक्ति को कुचलकर कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहेब निराश होकर नेपाल की ओर चला गया और वहीं कहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका साथी तात्या टोपे, झाँसी की रानी के साथ जा मिला।
5. लखनऊ में प्रमुख विद्रोही तथा नेता (Major Rebels – or Leaders at Lucknow): 30 मई, 1857 ई. को अवध की। राजधानी लखनऊ में विद्रोह की आग फैली। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में जनता एकत्रित हो गई जिससे इसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मौलवी मुहम्मदशाह, राजा मानसिंह, राजा हनुमंत सिंह और नवाब की बेगम हजरत महल ने भी महान सहयोग दिया।
हेनरी लारेंस को 1,000 अंग्रेज तथा 700 भारतीय सैनिकों सहित लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजीडेंसी में घेर लिया गया। हेनरी लारेंस को तोप का एक गोला लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात् हैवलाक, नील और कैंपबेल सेनाएँ लेकर लखनऊ की ओर चल पड़े। कई मास तक युद्ध चलता रहा। मार्च, 1858 ई. तक विद्रोहियों की शक्ति का पूरी तरह नाश कर दिया गया और लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लखनऊ के पतन के बाद विद्रोहियों के हौसले टूट गए।
6. बनारस और इलाहाबाद (Banaras and Allahabad) : दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार होने के पश्चात् बनारस और इलाहाबाद में भी विद्रोह हो गए थे। जनरल नौल (Neil) ने अंग्रेजों, सिक्खों तथा मद्रासी सैनिकों की सहायता से बनारस पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् वह। जून, 1857 ई. को इलाहाबाद पहुँच गया और यहाँ भी अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया।
7. मध्य भारत में झाँसी, ग्वालियर के समीपवर्ती क्षेत्र (Central India-Jhansi and Gwalior etc.) : मध्य भारत में झाँसी तथा ग्वालियर के समीपवर्ती क्षेत्र विद्रोह के मुख्य केंद्र बने रहे। 7 जून, 1857 ई. को झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झाँसी में क्रांति हुई। रानी ने अदम्य साहस, वीरता एवं कुशलता का परिचय दिया. और उसने झांसी पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया।
कानपुर के हाथों से निकल जाने के पश्चात् तात्या टोपे भी उसके साथ आ मिला। सर यूरोज की सेना ने विद्रोहियों को झाँसी और फिर कालपी में पराजित किया। जून, 1858 ई. में ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे का अधिकार हो गया। सर ह्यूरोज ने सिंधिया की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून, 1858 ई. को अंग्रेजों से संघर्ष करती हुई स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी पर न्यौछावर हो गई।

प्रश्न 3.
1857 के विद्रोह की असफलता के मुख्य कारण कौन-कौन से थे?
उत्तर:
विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे:
1. संगठन का अभाव (Lack of Organisation) : यह क्रांति सारे भारत की संगठित क्रांति न थी। इसमें संदेह नहीं कि क्रांति की चिनगारियाँ दूर-दूर तक गई थीं। फिर भी संगठन के अभाव के कारण देशव्यापी क्रांति नहीं हुई। भारतीयों में राष्ट्रीयता का भाव नहीं था। उत्तर-पश्चिम में अफगान शांत रहे। अफगानिस्तान के शासक दोस्त मुहम्मद ने संकटपूर्ण स्थिति होने पर भी उससे लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया। सिक्खों और गोरखों ने अंग्रेजों की सहायता की। भारत के देशी राजा राजभक्त बने रहे और अंग्रेजों के साथ बने रहे। सिंधिया, होल्कर, निजाम और राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की।
2. एक उद्देश्य का अभाव (Lack of Single Aim) : क्रांतिकारियों का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। सभी शासकों और जमींदारों के निजी स्वार्थ थे, जिनके लिए वे लड़ रहे थे। मुसलमान मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवन देना चाहते थे जबकि हिंदू लोग हिंदू राज्य की स्थापना के इच्छुक थे। बहादुरशाह द्वितीय दिल्ली पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। झाँसी की रानी अपनी झाँसी को बचाना चाहती थी, जबकि नाना साहेब अपनी पेंशन बचाने के लिए जूझ रहे थे। इस समय तक जन-साधारण राष्ट्रीयता की भावना से दूर था।
3. योग्य नेतृत्व का अभाव (Lackof Capable Commandership) : विद्रोहियों के पास योग्य सैनिक नेतृत्व का अभाव था जबकि अंग्रेजी सेनाओं का संचालन एक ही प्रधान सेनापति के अधीन नील, हैवलाक, आटम, युरोज, निकल्सन और लारेंस जैसे योग्य और अनुभवी जनरलों ने किया। क्रांतिकारियों का प्रधान सेनापति मिर्जा मुगल (बहादुर शाह द्वितीय का पुत्र) था जिसमें किसी प्रकार की सैनिक प्रतिभा न थी। विद्रोहियों में केवल झाँसी की रानी और तात्या टोपे योग्य सेनानी थे। अवध की बेगम हजरत महल और दिल्ली की सम्राज्ञी जीनत महल भी नरेशों और जागीरदारों से तालमेल न स्थापित कर सकीं। अत: विद्रोही बिना किसी निश्चित योजना के लड़ते रहे। उनकी शक्ति बिखरी हुई थी। इसको नष्ट करने में अंग्रेजों को अधिक समय नहीं लगा।
4. अंग्रेजों के उत्तम संसाधन (Good resources of the English): अंग्रेजों के साधन, विद्रोहियों के साधनों से अधिक उत्तम थे। उनके पास अनुशासित सेना और नवीनतम हथियार थे। उनके पास यातायात और संचार व्यवस्था थी, जबकि विद्रोहियों के पास ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति और तोपखाना अधिक उपयोगी थे।
5. अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा सहायता (Help to the English by the Indians) : क्रांतिकारियों में मुख्यतः सामंतवादी तत्त्व ही थे.कछ राष्ट्रवादी तत्त्व साथ तो थे, परंतु नहीं के बराबर। क्रांतिकारियों के नेता भी प्राय: सामंत ही थे। पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद और नेपाल के देशी राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की और उन्हें बड़ा सहयोग दिया। देशी राजाओं के अतिरिक्त सिक्खों और गोरखों ने भी अंग्रेजों की बड़ी सहायता की थी।
प्रश्न 4.
1857 के विद्रोह के प्रभाव एवं परिणामों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:
1857 के विद्रोह के प्रभाव एवं परिणाम :
1. कंपनी शासन की समाप्ति (End of the Rule of the Company): 1858 के अधिनियम एवं महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (नियंत्रक मंडल तथा संचालक मंडल) भी भंग कर दिए गए।
2. भारत का शासन सीधा इंग्लैंड की सम्राज्ञी या ताज के अधीन हो गया (India came under direct control of the Queen/ King of England) : भारत का शासन प्रबंध सीधा महारानी या ताज (क्राउन) के अधीन हो गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट (संसद) भारत के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च विधायिका बना दी गई। इंग्लैंड में रहने वाले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (या भारत सचिव) की नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी ने की। भारत सचिव ब्रिटेन के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट श्रेणी (रैक) का मंत्री होता था। उसकी सहायता के लिए वहीं 15 सदस्यों की एक काउंसिल (परिषद) गठित की गई। भारत सचिव इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
3. गवर्नर-जनरल वायसराय बना (Governor-General became Viceroy): अब तक भारत में गवर्नर-जनरल दिन प्रतिदिन के प्रशासन चलाने एवं भारतीय मामलों के लिए नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब उसके पद को नया नाम-वायसराय दिया गया। वायसराय का अर्थ था-राजा का प्रतिनिधि। इस तरह वायसराय सन् 1858 ई. से भारत में राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाने लगा। लेकिन उस पर सीधा समुद्री तार के माध्यम से भारत सचिव का नियंत्रण होता था। वह हर रोज उसे निर्देशन एवं मार्गदर्शन देता रहता था।
4. भारतीय नरेशों के प्रति नीति में बदलाव (Changes in the policy towards Indian Rulers):
- 1858 की महारानी की घोषणा में देशी रियासतों के शासकों को यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में किसी भी राज्य का भू-भाग या राज्य ब्रिटिश भारत साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा।
- जो-जो संधियाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी नरेशों से की थीं, उनका पूर्ण सम्मान इंग्लैंड की सरकार करेगी।
उन्हें (देशी राजाओं को) नि:संतान होने पर अपनी इच्छानुसार गोद लेने का अधिकार होगा।
5. सांप्रदायिक सद्भाव एवं हिंदू-मुस्लिम एकता की सुदृढ़ता (Communal Harmony and Unity among the Hindus and Muslims): 1857 के विद्रोह में भारत में दो प्रमुख संप्रदायों के लोगों (हिंदू-मुसलमान) ने एक सामान्य शत्रु अंग्रेजों का सामना किया था। उन्हें साथ-साथ तोपों पर बांधा गया, फाँसी दी गई, कैद किया गया। इससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एकता और भी सुदृढ़ हुई तथा संपूर्ण देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण व्याप्त हो गया।
जब जनता बगावत करती है (1857 और उसके बाद) Class 8 HBSE Notes
- सैनिक विद्रोह (बगावत) (Mutiny) : जब सिपाही एकत्र होकर अपने सैनिक अफसरों का आदेश मानने से इंकार कर देते हैं।
- फिरंगी (Firangis) : विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव छिपा होता है।
- कारतूस (Cartridge) : गोली रखने वाला खाली पुष्ट कागज।
- पैदल सेना (Infantry) : वे सिपाही जो पैदल चलते हुए लड़ते हैं।
- सिपाही (Sepoy) : कंपनी में भारतीय सैनिक या सेना।
- तालुकदार (Taluqdars) : छोटे भूमिस्वामी।
- जिहाद (Jihad) : पवित्र युद्ध (या क्रूसेड), जो मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा लड़ा जाता है।
- बहुपत्नी विवाह (Polygamy) : एक से ज्यादा पत्नियाँ रखने की प्रथा।
- वेल्लौर सैनिक बगावत (The Mutiny of Vellore) : यह बगावत 1806 ई. में हुई थी।
- बैरकपुर में सैनिक विद्रोह (The Mutiny at Barrackpore) : 1824 ई. में।
- फिरोजपुर में सैनिक बग़ावत (The Mutiny of Ferozepur) : फरवरी, 18421
- 7वीं बंगाल घुड़सवार सेना की बगावत हुई थी (The Mutiny of the 7th Bengal Cavalry) : 1849 में।
- 64वीं रेजीमेंट का सैनिक विद्रोह (The Mutiny of the 64th Regiment) : 1849 में।
- बरेली में बगावत उठी (The Bareilly rising) : 1816 में।
- कोल राजविद्रोह का काल (The Kol Insurrection) : 1831-32 ई.।
- कांगड़ा के राजाओं की बगावत (The Revolt of the Rajas of Kangra) : 1848
- जसवार एवं दातरपुर में संथाल विद्रोह हुआ (Santhal rising at Jaswar and Datarpur) : 1855-56 में।
- धार्मिक अयोग्यताएँ अधिनियम (The Religious Disabilities Act) : 1850 ई.।
- 22वीं नेटिव इन्फैन्ट्री की सैनिक बगावत (The Mutiny of the 22nd N.I.) : 18491
- 66वीं नेटिव इन्फैन्ट्री की बगावत (The Mutiny of the 66th N.I.) : 18501
- 38वीं नेटिव इन्फैन्ट्री का विद्रोह (The Mutiny of the 38th N.I.) : 1852।
- लार्ड कैनिंग का जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट (Lord Canning’s General Service Enlishment Act) : 18561
- 19वीं नेटिव इंफेंट्री का सैनिक विद्रोह बुरहानपुर में हुआ (Mutiny of the 19th Native Infantry at Burhanpur) : 2 फरवरी, 18571
- सतारा राज्य का विलय किया गया (The State of Satara was annexed in) : 1848।
- जैतपुर, बुंदेलखंड एवं संबलपुर का कंपनी भू-भाग में विलय हुआ : 18491
- उदयपुर का विलय हुआ : 18521
- नागपुर का विलय हुआ : 1853।
- झांसी का विलय हुआ : 18531
- मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा कंपनी सत्ता के विरुद्ध बगावत प्रारंभ : 10 मई, 18571
- दिल्ली, फ़िरोजपुर, बंबई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर आदि में विद्रोह फैलता चला गया : 11 मई से 30 मई 1857 के मध्य।
- ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, लखनऊ आदि में विप्लव : जून, 1857।
- इंदौर, महोव, झेलम एवं सियालकोट (पंजाब में) बगावत : जुलाई, 1857।
- दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा अधिकार हुआ : सितंबर, 18571
- सर कोलिन कैंपबैल ने कानपुर की लड़ाई में विजय प्राप्त की तथा तात्या टोपे बच निकलने में कामयाब हुआ : दिसंबर 1857।
- अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः अधिकार स्थापित किया : मार्च 1858।
- झांसी का पतन एवं अंग्रेजों की वहाँ विजय : अप्रैल, 18581
- बिहार में ताजा विद्रोह का फूट पड़ना तथा कुंवर सिंह द्वारा उसका नेतृत्व : अप्रैल, 18581
- भारत पर अंग्रेजी सत्ता की पुनः स्थापना तथा बगावत को कुचला गया : जुलाई से दिसंबर 1858 के मध्य।
- रानी लक्ष्मीबाई झांसी की लड़ाई में अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गई। : जून, 18581
![]()
![]()
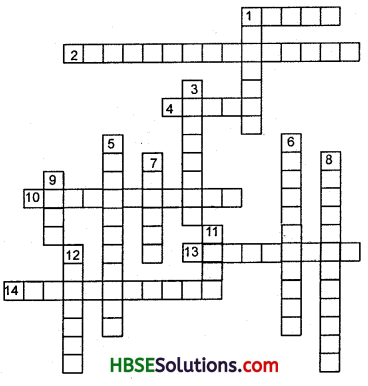
![]()
![]()