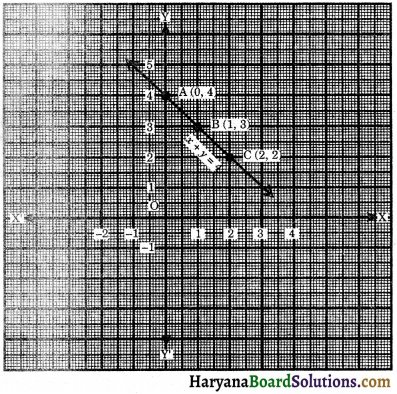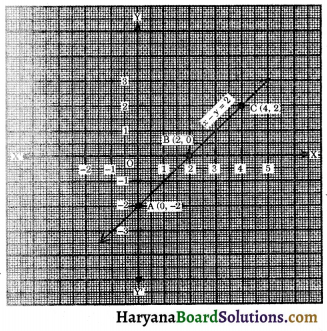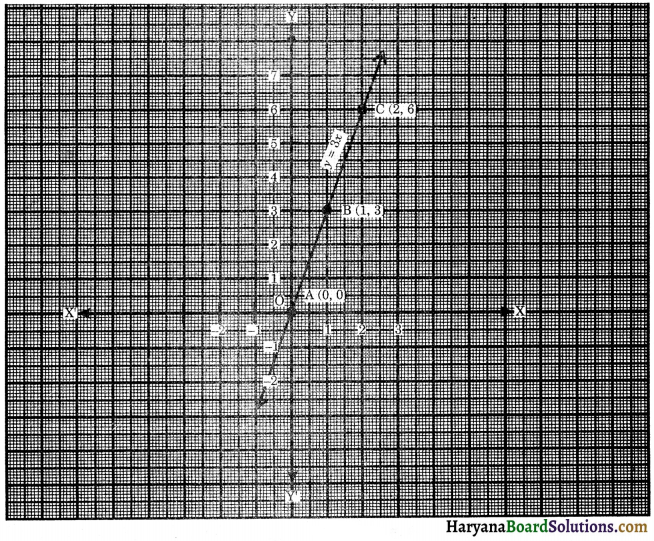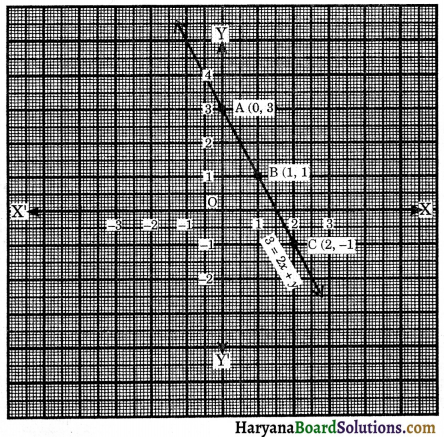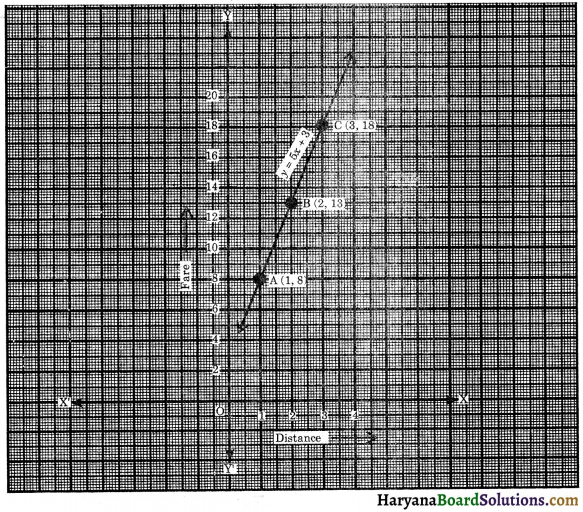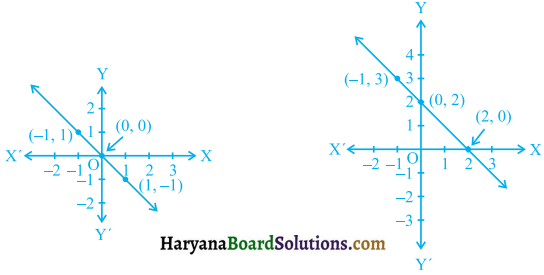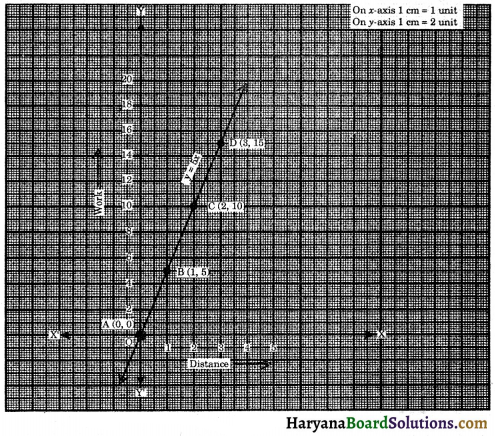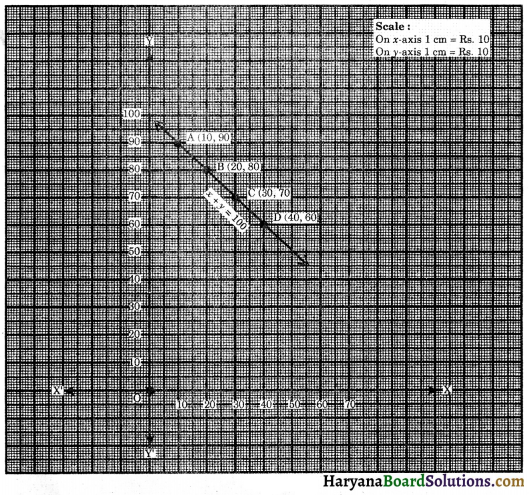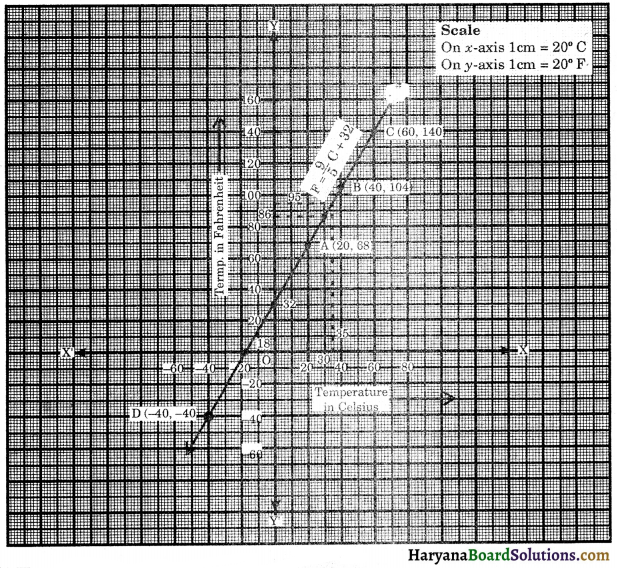Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 7 संघवाद Important Questions and Answers.
Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 7 संघवाद
अति लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
संघात्मक सरकार किसे कहा जाता है?
उत्तर:
संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है, जिसमें शासन की शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में बंटी हुई हों तथा प्रत्येक इकाई अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतन्त्र हो।
प्रश्न 2.
भारत के संविधान में संघ के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग किया गया है?
उत्तर:
भारत के संविधान में भारत के लिए ‘संघ’ के स्थान पर ‘राज्यों का संघ’ शब्द का प्रयोग किया गया है।
प्रश्न 3.
भारतीय संविधान के कोई दो संघात्मक लक्षण बताएँ।
उत्तर:
- भारतीय संविधान लिखित तथा कठोर है,
- संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा किया गया है।
प्रश्न 4.
भारतीय संविधान के कोई दो एकात्मक लक्षण बताइए।
उत्तर:
- संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने पर हमारा संघीय ढाँचा एकात्मक में बदल जाता है।
- भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए इकहरी नागरिकता के सिद्धान्त को अपनाया गया है।
प्रश्न 5.
भारत में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के कोई दो कारण बताएँ।
उत्तर:
- समस्त देश के आर्थिक विकास के लिए,
- स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय देशी रियासतों की समस्या तथा भारत की एकता व अखण्डता को बनाए रखना।
प्रश्न 6.
भारतीय संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को कितनी तथा कौन-सी सूचियों में बाँटा गया है? प्रत्येक सूची में दिए गए तीन-तीन विषय लिखिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटा गया है। ये हैं-
- संघीय सूची,
- राज्य सूची तथा
- समवर्ती सूची।
संघीय सूची में विदेशी मामले, प्रतिरक्षा व रेलवे, राज्य सूची में कृषि, पुलिस व जेलें तथा समवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह व तलाक आदि विषय शामिल हैं।
प्रश्न 7.
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है ?
उत्तर:
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमण्डल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा परस्पर विरोधी कानून बनाने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा।

प्रश्न 8.
अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) किसे कहते हैं? भारतीय संविधान द्वारा ये शक्तियाँ किसे दी गई हैं?
उत्तर:
अवशिष्ट शक्तियाँ वे विषय हैं जिनका वर्णन तीनों सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में से किसी में भी नहीं किया गया है। इन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है।
प्रश्न 9.
अन्तर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) की स्थापना क्यों तथा किसके द्वारा की जाती है?
उत्तर:
अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
प्रश्न 10.
पॉल एपलबी (Paul Appleby) ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को कैसी संघात्मक व्यवस्था का नाम दिया है?
उत्तर:
पॉल एपलबी (Paul Appleby) ने भारतीय संघवाद व्यवस्था को अत्यन्त संघात्मक (Extremely Federal) व्यवस्था का नाम दिया है।
प्रश्न 11.
सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ दी गई हैं और प्रत्येक में कितने विषय शामिल हैं?
उत्तर:
सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ-संघ सूची, समवर्ती सूची व राज्य सूची हैं। संघ सूची में मूलतः 97 विषय (वर्तमान में 100 विषय), समवर्ती सूची में मूलतः 47 (वर्तमान में 52 विषय) विषय तथा राज्य सूची में मूलतः 66 विषय (वर्तमान में 61 विषय) शामिल हैं।
प्रश्न 12.
समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं?
उत्तर:
समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं।
प्रश्न 13.
संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं ?
उत्तर:
संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे और वर्तमान में भी 100 विषय ही हैं।
प्रश्न 14.
राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं?
उत्तर:
राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं।
प्रश्न 15.
राज्य सूची में दिए गए किन्हीं दो विषयों के नाम बताइए।
उत्तर:
राज्य सूची में निम्नलिखित दो विषय हैं-
- कानून व शान्ति-व्यवस्था,
- कृषि।
प्रश्न 16.
समवर्ती सूची में दिए गए दो विषयों के नाम बताइए।
उत्तर:
समवर्ती सूची में निम्नलिखित दो विषय हैं-
प्रश्न 17.
केंद्र की आय के दो साधन बताइए।
उत्तर:
केंद्र की आय के दो साधन हैं-
प्रश्न 18.
राज्यों की आय के दो साधन बताइए।
उत्तर:
राज्यों की आय के दो साधन हैं
- बिक्री-कर
- कषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शल्क।
प्रश्न 19.
केंद्र व राज्यों के बीच तनाव के दो कारण बताइए।
उत्तर:
केंद्र व राज्यों के बीच तनाव के दो प्रमुख कारण हैं-
- राज्यपालों की भेदभावपूर्ण तथा विवादास्पद भूमिका,
- केंद्र द्वारा उन राज्यों के साथ भेदभाव किया जाना, जिनमें विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं।

प्रश्न 20.
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है और उसके क्या कार्य हैं?
अथवा
वित्त आयोग की स्थापना क्यों की जाती है? इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर:
वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग देश की वित्तीय व्यवस्था का परीक्षण करता है और केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के बारे में भी सिफारिश करता है।
प्रश्न 21.
केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनः विचार करने के लिए कब और किस आयोग की स्थापना की गई थी? अथवा सरकारिया आयोग की स्थापना कब और किस उद्देश्य के लिए की गई थी?
उत्तर:
9 जून, 1983 को केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनः विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री आर०एस० सरकारिया थे।
प्रश्न 22.
सरकारिया आयोग की कोई दो सिफारिशें बताइए।
उत्तर:
सरकारिया आयोग की दो प्रमुख सिफारिशें थीं-
- केंद्र को राज्यों में केंद्रीय पुलिस बल नियुक्त करने का अधिकार बना रहे,
- अन्तर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की जाए।
प्रश्न 23.
उन दो परिस्थितियों को बताएँ जिनमें कि संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है।
उत्तर:
संसद राज्य सूची पर दी गई दो परिस्थितियों में कानून बना सकती है-
- अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व समझौते लागू करने पर,
- जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्त्व को घोषित कर दे।
प्रश्न 24.
केंद्र व राज्यों के बीच दो विधायी सम्बन्ध बताइए।
उत्तर:
केंद्र व राज्यों के बीच दो विधायी सम्बन्ध इस प्रकार हैं-(1) समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, (2) राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है।
प्रश्न 25.
केंद्र व राज्यों के बीच दो वित्तीय सम्बन्ध बताइए।
उत्तर:
केंद्र व राज्यों के बीच दो वित्तीय सम्बन्ध इस प्रकार हैं-
- केंद्र राज्यों को अनुदान देता है,
- वित्तीय संकट की स्थिति में केंद्र राज्यों की आय के साधनों में परिवर्तन कर सकता है।
प्रश्न 26.
केंद्र व राज्यों के बीच दो प्रशासनिक सम्बन्ध बताइए।
उत्तर:
केंद्र व राज्यों के बीच दो प्रशासनिक सम्बन्ध इस प्रकार हैं-
- केंद्र राज्यों में केंद्रीय पुलिस बल भेज सकता है,
- राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य होते हैं।
प्रश्न 27.
केंद्र कब और किस आधार पर राज्य में आपात स्थिति लागू कर सकता है?
उत्तर:
केंद्र राज्य में संवैधानिक तन्त्र विफल हो जाने पर आपात स्थिति लागू कर सकता है। ऐसा केंद्र राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा बिना रिपोर्ट के भी कर सकता है।
प्रश्न 28.
केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार-विमर्श हेतु गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की?
उत्तर:
केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार-विमर्श हेतु गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 अक्तूबर, 1987 को प्रस्तुत की।
प्रश्न 29.
राज्य की स्वायत्तता की मांग के कोई दो कारण लिखें।
उत्तर:
राज्यों की स्वायत्तता की माँग के दो कारण इस प्रकार हैं-
- संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ,
- वित्तीय दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता।

प्रश्न 30.
राज्य स्वायत्तता के कोई दो साधन लिखें।
उत्तर:
राज्यों की स्वायत्तता के लिए विभिन्न सुझाए गए साधनों में दो निम्नलिखित हैं-
- संविधान में संघात्मक शासन का स्थापित किया जाना,
- राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक समिति का गठन हो जो उसे निष्पक्ष परामर्श प्राप्त करा सके।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
संघात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:
संघ जिसे अंग्रेजी में (Federation) अथवा (Federal) कहा जाता है, वास्तव में लैटिन भाषा के एक शब्द (Foedus) से बना है जिसका अर्थ है सन्धि अथवा समझौता। इस प्रकार संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थायी संगठन है, जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की जाती है। जब दो या अधिक स्वतन्त्र राज्य कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं तथा शेष उद्देश्यों की पूर्ति वे स्वयं करते हैं तो एक संघात्मक शासन की स्थापना हो जाती है।
प्रश्न 2.
संघात्मक सरकार के चार लक्षण बताएँ।।
उत्तर:
संघात्मक सरकार के चार लक्षण निम्नलिखित हैं
1. शक्तियों का बँटवारा संघात्मक सरकार में शक्तियों का बँटवारा होता है। महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास तथा स्थानीय महत्त्व की शक्तियाँ राज्य सरकारों को दी जाती हैं। दोनों इकाइयाँ अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं।
2. लिखित तथा कठोर संविधान संघ राज्य कई राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम होता है, इसलिए समझौते की सभी शर्ते लिखित रूप में होनी चाहिएँ। साथ ही ये शर्ते स्थायी हों, अतः संविधान लिखित तथा कठोर होता है।
3. स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के आपसी विवादों को निपटाने के लिए तथा कोई भी इकाई संविधान के विरुद्ध कानून न बना सके, इसके लिए एक स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है।
4. दो-सदनीय विधानपालिका-संघात्मक सरकार में दो-सदनीय विधानमण्डल की आवश्यकता होती है। विधानमण्डल का निम्न सदन राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है तथा ऊपरी सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रश्न 3.
संघात्मक सरकार के चार लाभ बताएँ।
उत्तर:
संघात्मक सरकार के चार मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं
1. शक्तिशाली राज्य की स्थापना-संघ सरकार स्थापित होने से छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली संघ राज्य कायम हो जाता है।
2. सरकार में अधिक कार्यकुशलता-संघ सरकार में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों तथा कार्य-क्षेत्रों का बँटवारा हो जाने से सरकारों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ जाती है।
3. बड़े राज्यों के लिए उपयोगी-संघ सरकार अधिक जनसंख्या तथा भिन्नता वाले राज्यों के लिए उपयुक्त है।
4. अधिक लोकतन्त्रीय संघ सरकार में लोकतन्त्र की संस्थाएँ अधिक तथा प्रत्येक स्तर पर संगठित की जाती हैं। इसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ लोगों को लोकतन्त्र का प्रशिक्षण देती हैं।
प्रश्न 4.
भारतीय संविधान संघात्मक है, स्पष्ट करो।
अथवा
भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का उल्लेख करें जो इसे संघीय स्वरूप प्रदान करते हैं।
अथवा
भारतीय संविधान की कोई पाँच संघीय विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर:
भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ (लक्षण) इस प्रकार हैं-
(1) भारतीय संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का तीन सूचियों में विभाजन किया गया है-
1. संघीय सूची (Union List), इस सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के मूलतः 97 विषय (वर्तमान में 100 विषय) हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति संघीय संसद के पास है।
2. राज्य सूची (State List) में मूलतः 66 विषय (वर्तमान में 61 विषय) हैं। ये विषय स्थानीय महत्त्व के हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमण्डलों को दिया गया है।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List), इस सूची में दिए गए मूल 47 विषयों (वर्तमान में 52 विषय) पर संसद तथा राज्य विधानमण्डल दोनों ही कानून बना सकते हैं,
(2) संविधान देश का सर्वोच्च कानून (Supremacy of the Constitution) है,
(3) भारतीय संविधान लिखित तथा कठोर है,
(4) संविधान की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है,
(5) संघीय विधानमण्डल (संसद) का गठन द्वि-सदनीय प्रणाली के आधार पर किया गया है। लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं।

प्रश्न 5.
भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पाँच कारण बताएँ।
उत्तर:
भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के कारण इस प्रकार हैं-
- ऐतिहासिक अनुभव के कारण संविधान के निर्माताओं ने शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की,
- तत्कालीन परिस्थितियों भारत का विभाजन, साम्प्रदायिक दंगों, तेलंगाना में सशस्त्र किसान आन्दोलन, भारतीय देशी रियासतों की समस्या इत्यादि ने भी संविधान निर्माताओं को प्रभावित किया,
- भारतीय आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु भी केंद्रीय शासन का शक्तिशाली होना अनिवार्य था,
- समस्त संसार में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है, भारत इसका कोई अपवाद नहीं है,
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतें मौजूद थीं। संविधान निर्माताओं ने देशी रियासतों की समस्या से निपटने के लिए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करने का निर्णय दिया।
प्रश्न 6.
केंद्र तथा राज्यों में कोई छह प्रशासनिक सम्बन्ध बताएँ।
उत्तर:
केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक सम्बन्ध इस प्रकार हैं-
- केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश तथा आदेश देने का अधिकार है,
- राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है,
- बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों को निर्देश दिया जाता है,
- राष्ट्रपति को प्रान्तीय संकट की घोषणा (अनुच्छेद 356) करने का अधिकार है,
- राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति अन्तर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है,
- राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निर्देश दे सकता है।
प्रश्न 7.
अर्द्ध-संघात्मक (Quasi-Federal) से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:
भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है, परन्तु पूर्ण संघात्मक नहीं, अर्द्ध-संघात्मक। अर्द्ध-संघात्मक से अभिप्राय है कि केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बँटवारा तो किया गया है, परन्तु शक्ति सन्तुलन केंद्र के पक्ष में है। संघ के अधिक शक्तिशाली होने के कारण भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्द्ध-संघात्मक कहा जाता है। प्रो० के०सी० व्हीयर के शब्दों में, “भारत का नया संविधान ऐसी शासन-व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक-से-अधिक अर्द्ध-संघीय है।”
प्रश्न 8.
राज्यों की स्वायत्तता पर संक्षेप में एक लेख लिखिए। .
उत्तर:
संविधान के लागू होने से लेकर अब तक केंद्र-राज्यों के सम्बन्धों में तनाव है। राज्य अधिक-से-अधिक स्वायत्तता की माँग करते रहे हैं तथा केंद्र के नियन्त्रण को कम करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ है कि राज्यों को अपने आन्तरिक क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता हो। संविधान द्वारा जो शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं, उनमें केंद्र हस्तक्षेप न करे।
प्रश्न 9.
संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है?
उत्तर:
ये परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं-
- देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने पर,
- यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में दिया गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का बन गया है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए,
- किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि अथवा समझौते को लागू करने के लिए,
- यदि दो अथवा दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास करके संसद को ऐसा करने की प्रार्थना करें,
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में उस राज्य के लिए।
प्रश्न 10.
वित्त आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
संविधान की धारा 280 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि देश की आर्थिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी। वित्त आयोग की स्थापना प्रायः 5 वर्ष के लिए की जाती है। इस आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ तथा नियुक्ति का तरीका निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग सरकार को दी गई कुछ बातों के बारे में परामर्श देता है
- संघ तथा राज्यों में राजस्व का विभाजन,
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा के बारे में,
- अन्य कोई भी मामला जो राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपा गया है। अब तक पन्द्रह (11 अप्रैल 2020 से) वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं।
प्रश्न 11.
‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार उन सब विषयों को, जिनका वर्णन किसी भी सूची अर्थात् संघीय सूची, राज्य सूची, अथवा समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों का नाम दिया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं।
प्रश्न 12.
सरकारिया आयोग पर संक्षेप में लेख लिखिए।
उत्तर:
सन् 1983 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने केंद्र व राज्यों के सम्बन्धों पर विचार करके रिपोर्ट देने के । लिए न्यायमूर्ति श्री आर०एस० सरकारिया के नेतृत्व में तीन-सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भारतीय संविधान के अन्तर्गत केंद्र तथा राज्यों के सम्बन्धों को ठोस बताया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। केवल कार्य-प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है और उन्हें ईमानदारी से लागू करना है। केंद्र सरकार ने इन सुझावों के आधार पर कोई ठोस कार्य नहीं किया।
प्रश्न 13.
योजना आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है, क्योंकि संविधान में इसकी स्थापना की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 15 मार्च, 1950 को एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी और 28 मार्च, 1950 से योजना आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था परन्तु 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद नवगठित भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इण्डिया (NITI) आयोग का गठन करने का निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप एक नई संस्था नीति (NITI-National Institute for Transforming India) का मार्ग प्रशस्त किया तथा 5 जनवरी, 2015 को इसकी नियुक्ति कर दी गई।
यद्यपि यहाँ हम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम के अनुसार योजना आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार योजना आयोग के स्वरूप, इसके कार्यों एवं भारत के विकास में योजना आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का भी संक्षेप में उल्लेख करेंगे एवं तत्पश्चात् नवगठित नीति आयोग की संरचना, उद्देश्यों एवं कार्यों पर भी संक्षेप में प्रकाश डालेंगे।
भारत में 1950 में कार्यरत योजना आयोग में प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होता था और वही इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता था। इसके अतिरिक्त आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती थी। उपाध्यक्ष पद पर देश के विख्यात अर्थशास्त्री या प्रसिद्धि प्राप्त वित्त विशेषज्ञ विराजमान रहे हैं।
यद्यपि उपाध्यक्ष मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता था परंतु उसका स्तर कैबिनेट मंत्री के समान होता था। उपाध्यक्ष वास्तव में योजना आयोग का सबसे प्रभावकारी अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन एवं भत्ते मिलते थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा योजना आयोग में 14-15 व्यक्ति और होते थे।
इनमें सात-आठ तो मंत्री शामिल थे; जैसे मानव संसाधन और विकास मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और योजना-राज्य मंत्री तथा पांच-छः अन्य सदस्य होते थे। सदस्यों में से कोई एक सदस्य आयोग के सचिव (Member Secretary) के रूप में कार्य करता था। आयोग के विशेषज्ञ सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था।
प्रश्न 14.
समवर्ती सूची पर एक नोट लिखिए।
उत्तर:
इस सूची में साधारणतः वे विषय रखे गए हैं, जिनका महत्त्व क्षेत्रीय व संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों, तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा।
इस सूची में वर्तमान समय में कुल 52 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं फौजदारी विषय, विवाह और विवाह-विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक-संघ, औद्योगिक विवाद, आर्थिक और सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व आदि। 42वें संवैधानिक संशोधन में 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा और नाप-तोल राज्य सूची में से समवर्ती सूची में परिवर्तित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची में एक नवीन विषय-‘जनसंख्या नियन्त्रण’ और ‘परिवार नियोजन’ रखा गया है।
प्रश्न 15.
केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव के पाँच कारण लिखें।
उत्तर:
केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव के पाँच कारण निम्नलिखित हैं-
(1) केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव का मुख्य कारण वित्त रहा है। राज्यों को हमेशा केंद्र से यह शिकायत रहती है कि वह सहायता देते समय भेदभावपूर्ण नीति अपनाता है,
(2) केंद्र व राज्यों के बीच तनाव का कारण राज्यपाल की भूमिका भी है। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से ऐसे राज्यों में जहाँ विरोधी दलों की सरकारें होती हैं, वहाँ राज्यपाल की भूमिका विवा का विषय बनी रहती है,
(3) नौकरशाही की भूमिका भी तनाव का अन्य कारण है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा किए जाने के कारण राज्य सरकारों का उन पर नियन्त्रण नहीं होता,
(4) कानून तथा व्यवस्था की समस्याएँ भी तनाव का कारण हैं, क्योंकि केंद्र शान्ति व व्यवस्था का बहाना लेकर राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है,
(5) दलीय भावना के कारण भी केंद्र राज्यों तथा राज्य केंद्र पर दोषारोपण करते रहते हैं, विशेष रूप से उस समय जब केंद्र में एक दल की सरकार हो तथा राज्य में किसी दूसरे दल की।

प्रश्न 16.
राज्य की स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? .
उत्तर:
राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ स्वतन्त्रता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्यों को उनके मामलों में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाना। राज्यों को जो शक्तियाँ संविधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं उन्हें उनका प्रयोग बिना किसी रोक-टोक के करने की आज्ञा होनी चाहिए। इस प्रकार राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ न तो राज्यों की स्वतन्त्रता से है और न ही प्रभुसत्ता से। यह एक ऐसा वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को कुछ क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता तथा कम-से-कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है। राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य के अधिकार का नाम ही राज्यों की स्वायत्तता है।
प्रश्न 17.
राज्य की स्वायत्तता की माँग के मुख्य कारणों का उल्लेख करो।
उत्तर:
राज्य की स्वायत्तता की माँग के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
- संसद की व्यापक विधि निर्वाण शक्तियाँ,
- वित्तीय दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता,
- अखिल भारतीय सेवाएँ तथा राज्यपाल,
- राज्यों के बीच भाषायी एवं सांस्कृतिक विभिन्नता,
- राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति शासन,
- अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े,
- राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व ।
प्रश्न 18.
भारतीय संविधान की कोई तीन एकात्मक विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान की तीन एकात्मक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
1. शक्तिशाली केंद्रीय सरकार-वैसे तो संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, परंतु इस विभाजन में केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। संघीय सूची में 97 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में केवल 66 विषय हैं। राज्य विषयों की संख्या ही कम नहीं, इनका महत्त्व भी कम है। जेलें, पुलिस तथा अन्य स्थानीय विषयों पर ही राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है।
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारें तथा केंद्रीय सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, परंतु मतभेद या विरोध की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा और राज्य विधानमंडल के कानून को रद्द कर दिया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) के विषय भी केंद्रीय सरकार को ही सौंपे गए हैं।
2. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। वह जिस राज्यपाल को जब चाहे, उसके पद से हटा सकता है। इस प्रकार गवर्नरों द्वारा भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के शासन-प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकती है।
3. राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन-संसद कानून पास कर किसी भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। वह दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है या एक राज्य को दो भागों में बाँट सकती है; जैसे पंजाब का विभाजन करके (पंजाब व हरियाणा) दो राज्य बनाए गए थे। यह अधिकार केंद्र को बहुत अधिक शक्ति देता है। इससे वह चाहे तो राज्यों पर निरंकुश होकर नियंत्रण कर सकता है।
निबंधात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
संघीय सरकार की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।
अथवा
संघ किसे कहते हैं? इसके आवश्यक लक्षणों का वर्णन कीजिए।
अथवा
संघात्मक सरकार की परिभाषा दीजिए तथा उसके गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।
अथवा
संघ क्या है? संघ की सफलता में सहायक अनिवार्य तत्त्वों का वर्णन कीजिए।
अथवा
संघात्मक सरकार की परिभाषा दें। एकात्मक तथा संघात्मक सरकार में भेद बतलाइए। अथवा संघ क्या होता है? एक अच्छे संघ के निर्माण के लिए कौन-से तथ्य सहायक होते हैं? अथवा संघ क्या होता है? भारत में कौन-सी सरकार उपयुक्त है?
उत्तर:
संघात्मक सरकार ऐसी शासन-व्यवस्था है, जिसमें शासन-सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया जाता है तथा जिसमें दोहरी सरकारें स्थापित की जाती हैं और उनकी शक्तियों का बँटवारा कर दिया जाता है।
संघ जिसे अंग्रेज़ी में ‘Federation’ अथवा ‘Federal’ कहा जाता है, वास्तव में लैटिन भाषा के एक शब्द ‘फोडस’ (Foedus) से बना है जिसका अर्थ है ‘सन्धि अथवा समझौता’ । इस प्रकार संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थायी संगठन है, जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की जाती है। जब दो अथवा दो से अधिक स्वतन्त्र राज्य कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं तथा शेष उद्देश्यों की पूर्ति वे स्वयं करते हैं तो एक संघात्मक शासन की स्थापना हो जाती है। विभिन्न विद्वानों ने संघ सरकार की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं
1. मॉण्टेस्क्यू (Montesquieu):
के शब्दों में, “संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहाँ बहुत-से एक जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हों।”
2. हेमिल्टन (Hemilton):
का कथन है, “संघ राज्य, राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य की स्थापना करता है।”
3. गार्नर (Garner):
का कथन है, “संघ सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें संविधान द्वारा अथवा संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं।”
4. जेलीनेक (Jelineck):
के अनुसार, “संघात्मक राज्य कई राज्यों के मेल से बना हुआ एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है।”
5. फाइनर (Finer):
के शब्दों में, “संघात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्ति का कुछ भाग स्थानीय राज्यों को दिया जाए, दूसरा भाग संघात्मक सरकार को दिया जाए जो कि अपने स्थानीय राज्यों की इच्छा से बनी होती है।”
इन परिभाषाओं के आधार पर संघात्मक सरकार वह शासन-प्रणाली है, जिसमें कई स्वतन्त्र राज्य मिलकर समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संघ स्थापित कर लेते हैं। इस संघ में प्रत्येक सदस्य-राज्य कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखता है तथा सामान्य हित के विषयों को एक केंद्रीय सत्ता के सुपुर्द कर देता है। संघात्मक सरकार के लक्षण (Features of Federal Government)-संघात्मक सरकार के आवश्यक लक्षण अथवा विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. लिखित, कठोर तथा सर्वोच्च संविधान संघ राज्य कई राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम होता है, इसलिए समझौते की सभी शर्ते लिखित रूप में होनी चाहिएँ। साथ ही ये शर्ते स्थायी भी हों। इसलिए संघ सरकार का संविधान केवल लिखित ही नहीं, कठोर भी होता है, जिससे कोई भी इकाई मनमाने ढंग से इसमें परिवर्तन न कर सके। संविधान सर्वोच्च भी होता है ताकि कोई भी सरकार उस संविधान के विरुद्ध कानून बनाकर दूसरी इकाई के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सके।
2. शक्तियों का बँटवारा-संघात्मक सरकार में केंद्रीय महत्त्व के विषय केंद्रीय सरकार को तथा प्रान्तीय और स्थानीय महत्त्व के विषय राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में कानून बनाती तथा प्रशासन चलाती हैं। वे एक-दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करतीं। भारत में शक्तियों के विभाजन के अधीन तीन सूचियाँ केंद्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची बनाई गई हैं।
3. स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका-संघात्मक शासन में एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र संघीय न्यायालय का होना भी जरूरी है। संघ सरकार में यद्यपि केंद्र व राज्यों में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, फिर भी उनमें कई बातों में विवाद होना स्वाभाविक है। संघ न्यायालय उनके विवादों को हल करता है। यह न्यायालय संविधान के संरक्षण का भी कार्य करता है। केंद्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें संविधान के विरुद्ध कानून न बना सकें, इसके लिए एक स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है।
4. द्वि-सदनीय विधानपालिका-संघात्मक सरकार में द्वि-सदनीय विधानमण्डल की आवश्यकता पड़ती है। विधानमण्डल का निम्न सदन सारे राष्ट्र की जनता का तथा उच्च सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपरी सदन राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। इसमें संघ की इकाइयों को बराबर सीट देने की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनकी संवैधानिक समानता स्थापित हो सके।
5. दोहरा शासन-संघात्मक सरकार में दोहरा शासन-प्रबन्ध होता है। एक केंद्रीय शासन तथा दूसरा स्थानीय अथवा प्रान्तीय शासन। संघ तथा प्रान्तों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित होते हैं। दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं।
6. दोहरी नागरिकता-संघ सरकार में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक उस राज्य की नागरिकता जहाँ वह निवास करता है, तथा दूसरी संघ की नागरिकता। ऊपर वर्णित तत्त्व संघीय सरकार के निर्माण में आवश्यक हैं। इन तत्त्वों के आधार पर ही संघात्मक सरकार की स्थापना होती है।

प्रश्न 2.
“भारतीय संविधान का स्वरूप या ढाँचा संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए।
अथवा
भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ बताएँ। भारतीय संविधान में दिए गए एकात्मक तत्त्वों का विवरण दो।
उत्तर:
26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर अधिकांश विद्वानों तथा राजनेताओं ने इसे एक आवाज में संघात्मक संविधान माना। फिर भी संविधान का संघात्मक ढाँचा विद्वानों में हमेशा विवाद का विषय रहा है। एक ओर प्रो० अलैक्जेण्ड्रोविक्स, के० संथानम, मोरिस जोन्स, एम०वी० पायली, डॉ० अम्बेडकर, पाल एपेल्बी आदि विद्वान् और राजनेता .. भारतीय संविधान को संघात्मक मानते थे तो दूसरी ओर कुछ विचारक इस बात से सहमत नहीं थे।
प्रो० अलेक्जेण्ड्रोविक्स के शब्दों में, “भारत निस्सन्देह एक संघ है जिसमें प्रभुसत्ता के तत्त्वों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है।” डॉ० के०सी० व्हीयर, जेनिंग्ज, डी०डी० बसु, डी०एन० बैनर्जी, के०पी० मुखर्जी, के०वी० राव आदि भारत के संविधान को संघात्मक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। के०पी० मुखर्जी के अनुसार,
“भारतीय संविधान निश्चय ही गैर-संघात्मक या एकात्मक संविधान है।” इसी तरह के०सी० व्हीयर का कहना है, “भारतीय संविधान अर्द्ध-संघात्मक है। वह नाममात्र की एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक राज्य होने के बजाय गौण संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है।” कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों तरह के तत्त्व पाए जाते हैं।
इस तरह भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। भारतीय संविधान के संघात्मक तत्त्व (Federal Elements of Indian Constitution)-भारतीय संविधान में निम्नलिखित संघात्मक तत्त्व मौजूद हैं
1. लिखित संविधान भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। 9 दिसम्बर, 1946 में संविधान का कार्य आरम्भ हुआ तथा 26 नवम्बर, 1949 में संविधान पूरा हुआ। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जिन्हें 12 अनुसूचियों और 22 अध्यायों में बाँटा गया है। भारतीय संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं।
2. संविधान की कठोरता भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। यद्यपि भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह कठोर तो नहीं है, परन्तु फिर भी इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं रखी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 ने भी इसीलिए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद का 2/3 बहुमत तथा केंद्र-राज्यों के सम्बन्धों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली व्यवस्थाओं पर आधे राज्यों के अनुमोदन के साथ संसद के दो-तिहाई बहुमत का जटिल तरीका अपनाया गया है।
3. संविधान की सर्वोच्चता भारत में संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है। यदि किसी समय केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र के किसी मामले पर विवाद हो तो उसका हल संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही निकाला जाएगा। अमेरिका आदि संघीय संविधानों की तरह भारत में भी यही तरीका अपनाया गया है।
4. शक्तियों का विभाजन-भारत में संघीय शासन के अन्तर्गत शक्तियों को केंद्र तथा राज्यों में बाँटा गया है। इस उद्देश्य के लिए तीन सूचियाँ (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) बनाई गई हैं। संघ सूची में 97 विषय (वर्तमान में 100 विषय), राज्य सूची में 66 विषय (वर्तमान में 61 विषय) तथा समवर्ती सूची में 47 विषय (वर्तमान में 52 विषय) रखे गए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई हैं।
राष्ट्रीय महत्त्व के विषय, यथा-देश की सुरक्षा, संचार साधन, विदेश-नीति, मुद्रा, बैंकिंग आदि महत्त्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए हैं। पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि विषय राज्य सूची में रखे गए हैं। दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं, परन्तु इस सूची पर सर्वोच्चता केंद्र सरकार को दी गई है।
5. दोहरी शासन-प्रणाली-भारत में दोहरी शासन-प्रणाली अपनाई गई है। केंद्र तथा राज्यों की अलग-अलग सरकारें हैं। दोनों को शासन की शक्तियाँ संविधान ने दी हैं। यद्यपि सहकारी संघवाद के कारण दोनों सरकारें आपस में सहयोग करके अपने-अपने दायरे में शासन चलाती हैं, फिर भी दोनों में से कोई किसी के अधीन नहीं हैं।
6. न्यायपालिका की विशेष स्थिति-संघ-शासन में केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र के विवाद को संविधान में की गई. व्यवस्थाओं के आधार पर निपटाने की शक्ति न्यायपालिका को दी जाती है। इस आधार पर भारत में भी न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करता है। इसके निर्णय अन्तिम होते हैं।
7. दो-सदनीय विधानमण्डल-संघ शासन में दो-सदनीय विधानमण्डल होता है। एक सदन सारे देश का तथा दूसरा सदन उन इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जो मिलकर संघीय सरकार का निर्माण करती हैं। भारत में लोकसभा सारे देश का तथा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह व्यवस्था इसलिए की जाती है, जिससे केंद्र सरकार राज्यों के हितों को नुकसान न पहुँचा सके।
संविधान में एकात्मक तत्त्व (Unitary Elements of Indian Constitution)-भारतीय संविधान में संघ शासन की इन आधारभूत विशेषताओं के होते हुए भी एकात्मक तत्त्वों की कमी नहीं है। भारत के संविधान में निम्नति
1. इकहरी नागरिकता भारत में अमेरिका के विरुद्ध इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे (जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर) वह राज्य का नहीं, भारत का नागरिक है। इकहरी नागरिकता की यह व्यवस्था संघ शासन के विरुद्ध है।
2. केंद्र तथा राज्यों के लिए एक संविधान-संघ शासन वाले राज्यों में संघ की इकाइयों को अलग-अलग संविधान बनाने का अधिकार होता है। अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड तथा अन्य संघीय देशों में यही तरीका अपनाया गया है। लेकिन भारत में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है। पूरे देश पर एक ही संविधान लागू होता है।
3. शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है, यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर दे, राज्य स्वयं कानून बनाने की प्रार्थना करे अथवा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, परन्तु विवाद की दशा में केंद्र का कानून लागू होगा। ऐसी दशा में केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।
4. अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास आमतौर पर संघ शासन में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, लेकिन भारतीय संविधान में साफ तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि जो विषय तीनों सूचियों में नहीं हैं ऐसे सभी अवशिष्ट विषयों पर संसद कानून बनाएगी, राज्यों के विधानमण्डल नहीं।
5. राज्यपालों की नियुक्ति-भारतीय संघ के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजता है तथा किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल बढ़ाता है अथवा पाँच वर्ष की अवधि से पहले हटाता भी है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमन्त्री से परामर्श लिया जाता है, परन्तु उस परामर्श को मानना आवश्यक नहीं है। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राज्य के प्रति नहीं, वरन् राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यह संघात्मक गुणों के विपरीत है।
6. राज्यों में राष्ट्रपति शासन-राष्ट्रपति राज्यपाल के सुझाव अथवा स्वयं निर्णय करके किसी भी राज्य में वहाँ की विधिवत निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लाग कर सकता है। ऐसी दशा में शासन की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं।
7. राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व-अमेरिकी सीनेट की तरह संघ शासन वाले देशों में केंद्रीय विधानमण्डल के ऊपरी सदन में सभी राज्यों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होते हैं, परन्तु भारत में इस सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया है। राज्यसभा में राज्यों को उनकी आबादी के अनुसार स्थान दिए गए हैं। जिस कारण राज्यसभा अधिक प्रभावशाली बनकर राज्यों के हितों की पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकती।
8. संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार संघ शासन में केंद्रीय विधानमण्डल सम्बन्धित राज्य की इच्छा के बिना उसकी सीमाओं तथा नामों आदि में परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन भारत में संसद को यह अधिकार दिया गया है।
सन् 1956 में केंद्र ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया, जिसके अधीन कितने ही नए राज्य बनाए गए हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किए गए हैं तथा उनके नामों में भी परिवर्तन किए गए हैं। इसी आधार पर के०पी० मुखर्जी ने लिखा है, “अगर एकात्मक सरकार की परिभाषा यह नहीं है तो मैं नहीं जानता कि वह क्या है।”
9. इकहरी न्याय पद्धति संघ शासन में न्याय व्यवस्था दोहरी होती हैं, परन्तु भारत में नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका का ढाँचा एकीकृत है। उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका के शिखर पर है। इसके साथ ही पूरे देश के लिए एक जैसी दीवानी तथा फौजदारी व्यवस्था है।
में राज्य केंद्र पर आश्रित केंद्र की अपेक्षा राज्य सरकारों की आय के साधन बहुत कम हैं। इसलिए राज्यों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। अनेक केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व का राज्यों में वितरण किया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं और नीति आयोग के निर्देशन में पूरे राष्ट्र के सुनियोजित विकास की व्यवस्था ने राज्यों को केंद्र पर निर्भर बना दिया है।
11. नीति आयोग पर केंद्र का प्रभुत्व (Dominance of Centre on NITI Commission)-1 जनवरी, 2015 को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आए नीति आयोग पर भी केंद्र का ही प्रभुत्व है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी योजना आयोग की तरह प्रधानमन्त्री होगा तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमन्त्री करता है। इसके अतिरिक्त दो पूर्वकालिक सदस्यों की नियुक्ति भी प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है। इसके साथ-साथ समय-समय पर विशिष्ट सदस्यों को भी प्रधानमन्त्री द्वारा ही आमन्त्रित किया जाता है।
पदेन सदस्यों में भी केंद्रीय मन्त्री ही सम्मिलित होते हैं। नीति आयोग में उल्लेखित प्रशासनिक परिषद् में यद्यपि राज्यों के मुख्यमन्त्री सदस्य होंगे परन्तु इसकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी प्रधानमन्त्री द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि नवगठित नीति आयोग में केंद्र का ही प्रभुत्व बना हुआ है जो भारतीय शासन को एकात्मकता की ओर झुकाता है।
निष्कर्ष-उपरोक्त संघात्मक एवं एकात्मक तत्त्वों का अध्ययन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः एकात्मक है और न ही संघात्मक। डॉ० जैनिंग्ज के अनुसार, यह कहना उचित होगा कि, “भारत सशक्त केंद्रीयकरण वाली विशेषताओं से युक्त संघ है।”
प्रश्न 3.
केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी सम्बन्धों का वर्णन करें। अथवा केंद्र राज्यों की वित्तीय जरूरतों को कैसे पूरा करता है? स्पष्ट करें। अथवा केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण दो।
अथवा
भारत में संघ तथा राज्यों के आपसी सम्बन्धों का संक्षेप में वर्णन करें।
उत्तर:
भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत शासन की शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटा गया है और अवशेष शक्तियाँ केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। भारत में पूर्णतः संघात्मक सरकार नहीं है और जिन देशों में पूर्ण संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है, उन देशों में भी केंद्र का राज्यों पर प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है तथा राज्यों की भी केंद्र पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारत में केंद्र अथवा संघ सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के आपसी सम्बन्धों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है
- विधायी सम्बन्ध,
- प्रशासनिक सम्बन्ध,
- वित्तीय सम्बन्ध ।
1. केंद्र तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध (Legislative Relation between Centre and States) भारतीय संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग के अध्याय एक में अनुच्छेद .245 से 254 तक में दिया है।
(1) संघ सूची इस सूची में संविधान लागू होते समय मूलतः 97 विषय (वर्तमान में 100 विषय) रखे गए है। इनमें प्रतिरक्षा, अणुशक्ति, विदेशी मामले, युद्ध और सन्धि, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, डाक- तार आदि विषय शामिल हैं। संघ सूची में इन सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है और उन पर केंद्र सरकार का ही प्रशासनिक नियन्त्रण कायम है।
(2) राज्य सूची इस सूची में मूल रूप से 66 विषय (वर्तमान में 61 विषय) रखे गए हैं। राज्य सूची में पुलिस, जेल, न्याय . प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन आदि शामिल हैं। समय-समय पर संविधान संशोधनों द्वारा इस सूची में विषयों को निकाला तथा जोड़ा जाता रहा है, परन्तु मूल रूप में इनकी संख्या 66 ही रही है। इस सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है तथा उन पर उनका ही प्रशासनिक नियन्त्रण कायम रहता है।
(3) समवर्ती सूची-इस सूची में मूल 47 विषय (वर्तमान में 52 विषय) रखे गए हैं। इनमें फौजदारी कानून, निवारक नजरबंदी कानून, विवाह, तलाक, ट्रेड यूनियन, श्रम, कल्याण, खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्यों को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है, ऐसे सभी मामलों पर अवशिष्ट अधिकार के रूप में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है।
संसद द्वारा राज्य-सूची पर कानून निर्माण-यद्यपि राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का – है, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है-
(1) यदि राज्यसभा अपने उपस्थित स्यों के बहमत और कल सदस्य संख्या के 2/3 बहमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर दे,
(2) राष्ट्रपति देश में संकटकाल की घोषणा कर दे,
(3) अगर दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की अपील करें,
(4) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों तथा समझौतों को लागू कराने के लिए संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है,
(5) राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। तब उस राज्य के लिए राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है,
(6) राज्यपाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेज सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा उसे रोक सकता है,
(7) राज्य सरकारों को एक राज्य से दूसरे राज्यों अथवा संघ प्रशासित क्षेत्रों से आने वाली वस्तुओं या उनके व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित मामलों पर युक्तिसंगत प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसा विधेयक विधानमण्डल में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है।
इस विवरण से स्पष्ट है कि विधायी क्षेत्र में राज्य सूची में दिए गए मामलों पर भी केंद्र सरकार को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, परन्तु विवाद की दशा में राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा, वरन् केंद्रीय संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा।
2. केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध (Administrative Relation of Centre and State) भारतीय संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को जिन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया है, उन्हीं मामलों पर उसने उन्हें अपना प्रशासनिक नियन्त्रण कायम करने की शक्ति भी दी है। संविधान में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण दिया गया है, जो इस प्रकार है
(1) संविधान के अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस तरह करेंगी जिससे संसद के कानूनों का पालन होता रहे,
(2) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने के बारे में जरूरी निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार नदियों, जलाशयों और महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मार्गों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है तथा रेलवे सम्पत्ति के संरक्षण के बारे में निर्देश दे सकती है,
(3) राष्ट्रपति ऐसे किसी भी कार्य को केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी को सौंप सकता है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है,
(4) केंद्र तथा राज्य सरकारें न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करेगी और इस बारे में आवश्यक कानून संसद द्वारा बनाए जाएँगे,
(5) नदियों के पानी के प्रयोग, वितरण और नियन्त्रण के मामलों पर संसद कानून बना सकती है तथा उस बारे में राज्यों के बीच विवाद होने पर मामले को मध्यस्थ या पंच के द्वारा हल करने के निर्देश केंद्र सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों को दे सकती है,
(6) भारतीय संघ के राज्यों के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान ने केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति को अन्तराज्यीय-परिषद् (Inter-state Council) कायम करने की शक्ति दे रखी है,
(7) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होने के साथ सम्बन्धित राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। अतः उसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन को प्रभावित करती है,
(8) केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। ऐसे आयोगों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर या अपनी ओर से भी इन वर्गों के कल्याण के लिए निर्देश देने का अधिकार राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार को प्राप्त है। ऊपर वर्णित विवरण से स्पष्ट है कि प्रशासनिक सम्बन्धों के मामलों में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार की स्थिति बहुत अधिक प्रभावशाली है।
3. केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध (Financial Relations between Centre and State Relation)-संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों की भी व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत वित्तीय मामलों में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है
(1) संघ तथा राज्यों की आय के साधन-संविधान के अनुसार संघ तथा केंद्र सरकार की आय के मुख्य साधनों में आय-कर, आयात व निर्यात-कर, सीमा शुल्क, समाचार-पत्रों की बिक्री तथा विज्ञापन पर कर, शराब तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर, सम्पत्ति शुल्क, डाक, टेलीफोन से प्राप्त आय आदि शामिल हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार की आय के प्रमुख साधनों में कृषि से होने वाली आय पर कर, शराब तथा ऐसी अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर, कृषि पर सम्पदा शुल्क, बिक्री-कर, बिजली के उपभोग पर कर, आमोद-प्रमोद के साधनों पर कर, वाहनों पर कर आदि शामिल किए गए हैं।
(2) करों के वितरण की व्यवस्था केंद्र की तुलना में राज्यों की आय के स्रोत बहुत कम हैं। राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि सुविधाओं के लिए धन की बहुत जरूरत पड़ती है। इसीलिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि कुछ कर ऐसे होंगे जिन्हें लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार को होगा, लेकिन इन करों से होने वाली आय को केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य : सरकारें अपने-अपने राज्यों में इकट्ठा करेंगी और वे ही उसे खर्च करेंगी।
इन करों में स्टाम्प शुल्क, दवाइयों और शृंगार की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क आदि शामिल हैं। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार कर लगाएगी और वसूली करेगी, परन्तु आय का कुछ भाग राज्यों को दिया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों पर उत्तराधिकार कर, रेल-भाड़े और माल-भाड़े पर लगने वाला कर, समाचार-पत्रों पर बिक्री तथा विज्ञापन कर, आय-कर, पटसन तथा जूट के निर्यात पर कर आदि शामिल हैं।
(3) राज्यों को अनुदान-ऊपर वर्णित वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त संविधान में व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय अनुदान या आर्थिक सहायता देगी। इनके अन्तर्गत राज्य सरकारें केंद्र से विकास की नई परियोजनाओं और दूसरे विकास कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। इसी तरह बाढ़, भूकम्प, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं की हालत में पीड़ित जनता की सहायता के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। आदिम जातियों और कबीलों की उन्नति के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। पूर्वोत्तर भारत में अनुसूचित क्षेत्रों की उन्नति तथा विकास के लिए केंद्र सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देती है।
(4) ऋण-संविधान ने केंद्र तथा राज्य सरकारों को ऋण लेने का अधिकार भी दे रखा है। केंद्र सरकार अपनी संचित निधि की जमानत पर संसद की अनुमति से देशवासियों तथा विदेशी सरकारों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय इकाइयों से ऋण ले सकती है। राज्य सरकारें देशवासियों तथा केंद्र सरकार से ही ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
(5) वित्तीय संकटकाल में केंद्र तथा राज्यों के सम्बन्ध-संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत राष्ट्र की वित्तीय साख अथवा वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो जाने की दशा में राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के परिणामस्वरूप राज्यों के आर्थिक मामलों में केंद्र सरकार को निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है। राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पास किए गए धन सम्बन्धी विधेयकों और प्रस्तावों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी जरूरी हो जाती है।
(6) वित्त आयोग-संविधान के अनुसार संविधान के लागू होने के दो साल के अन्दर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग (Finance Commission) गठित करेगा और फिर हर पाँच वर्ष बाद एक नया वित्त आयोग कायम किया जाएगा। आयोग में अध्यक्ष समेत पाँच सदस्य होंगे। यह आयोग केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के बारे में निर्णय करके अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को पेश करता है।
(7) भारत का नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक-संविधान ने पूरे देश के लिए एक नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था की है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह महालेखा परीक्षक केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखा-जोखा की निष्पक्ष तरीके से जाँच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद में प्रति वर्ष पेश करता है।
(8) योजना आयोग-योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, फिर भी संसद के 15 मार्च, 1950 को पास किए गए एक कानून के अनुसार उसे कायम किया गया था। देश के सम्पूर्ण सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी और वही उस सम्बन्ध में योजना का प्रारूप तैयार करता था। इस आयोग की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करता है। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है।

प्रश्न 4.
संघ (केंद्र) तथा राज्यों के बीच सम्बन्धों की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
उत्तर:
संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, वह संघ के पक्ष में है अर्थात् संघीय सरकार को राज्य सरकारों के मुकाबले में बहुत ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ऐसा होने पर भी सन् 1967 तक केंद्र तथा राज्यों के सम्बन्ध अच्छे रहे और उनमें किसी प्रकार का संघर्ष अथवा तनाव (Tension) उत्पन्न नहीं हुआ।
इसका मुख्य कारण था केंद्र तथा राज्यों में एक ही राजनीतिक दल अर्थात् काँग्रेस दल की सरकारों का होना। सन् 1967 के चुनावों के पश्चात् केंद्र में तो पुनः काँग्रेस दल की सरकार की स्थापना हुई, परन्तु कई राज्यों-बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु आदि में गैर-काँग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। इन सरकारों ने राज्यों को और अधिक शक्तियाँ देने की माँग की, जिससे केंद्र तथा राज्यों में संघर्ष आरम्भ हो गया। संघ तथा राज्यों के बीच संघर्ष अथवा तनाव के मुख्य कारण निम्नलिखित रहे हैं और आज भी हैं
1. वित्तीय समस्या केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव का एक मुख्य कारण वित्त रहा है। राज्य सरकारों को सदा यह शिकायत रहती है कि उन्हें जन-कल्याण के अनेक कार्य करने पड़ते हैं और उनकी आय के साधन बहुत कम हैं, इस कारण से उन्हें केंद्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र राज्यों को सहायता देते समय राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों के साथ पक्षपात करता है। अतः अधिकतर राज्यों की यह माँग रहती है कि उनकी आय के साधनों में वृद्धि की जाए, ताकि वित्त के मामले में उनकी केंद्र पर निर्भरता कुछ कम हो।
2. राज्यपाल की भूमिका केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटाने की भी शक्ति रखता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। पिछले कुछ समय से राज्यपाल की भूमिका के बारे में देश में काफी विवाद रहा है। विशेष रूप से ऐसे राज्यों में जहाँ विरोधी दलों की सरकारें बनी हैं। इस विवाद का एक मुख्य प्रश्न यह रहा है कि राज्यपाल को किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए।
3. नौकरशाही की भूमिका भारत में राज्यों के उच्च अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (I.A.S.) के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं, जिन पर राज्य सरकारों का पूरा नियन्त्रण नहीं होता। उनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए राज्य सरकारों की यह माँग रही है कि उन सभी कर्मचारियों पर, जो राज्य में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार का ही नियन्त्रण होना चाहिए। परन्तु अभी स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है।
4. कानून तथा व्यवस्था की समस्याएँ-संविधान के अनुसार कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परन्तु केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल भेज सकती है। राज्य सरकारों का यह विचार रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यों में सशस्त्र सेनाएँ तभी भेजनी चाहिएँ जब राज्य द्वारा ऐसी माँग की जाए, परन्तु व्यवहार में केंद्र ने कई बार अपनी इस शक्ति का प्रयोग राज्य की इच्छा के विरुद्ध किया है।
5. संकटकालीन प्रावधान-संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्रीय सरकार राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। इस प्रावधान का प्रयोग राज्य में “सवैधानिक तन्त्र की विफलता” (Failure of Constitutional Machinery in the State) की स्थिति में होता है। यह कदम राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम सन् 1959 में केरल में ई०एम०एस० नम्बूदरिपाद की सरकार को निलम्बित करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
उसके बाद लगभग सभी राज्यों को किसी-न-किसी कारण से राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत रहना पड़ा है। जिन राज्यों में विरोधी दल की सरकार को बर्खास्त किया जाता है, उनके द्वारा केंद्र पर सदा ही पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। इसी प्रकार सन् 1989 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन का लागू किया जाना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है।
सन् 1997 में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रोमेश भण्डारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करना भी एक ऐसा ही उदाहरण है। इस कारण से राज्य सरकारों ने प्रायः यह कहा है कि संवैधानिक तन्त्र की विफलता के प्रावधान की व्याख्या केंद्र ने समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार से की है।
6. दलीय कारण-दलीय भावना के कारण भी केंद्र राज्यों पर तथा राज्य केंद्र पर दोषारोपण करते रहते हैं, विशेष रूप से उस समय जब केंद्र में एक दल की सरकार हो तथा राज्य में किसी दूसरे दल की।
7. केंद्रीय कानूनों का कार्यान्वन-संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 केंद्र को यह अधिकार देते हैं कि वह राज्य सरकारों को संसद के कानून के अनुसार कार्य करने तथा राज्य के कार्यकारी अधिकारों के प्रयोग के बारे में आदेश दे। अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में भी उन्हें आदेश दिए जा सकते हैं। ऐसे कई आदेश राज्य सरकारों द्वारा अस्वीकार भी कर दिए जाते हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
8. अन्य फुटकर कारण-इस श्रेणी में राज्यों की सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण, भाषा का विवाद तथा नदियों के जल के बँटवारे से सम्बन्धित प्रश्न शामिल हैं। कई बार केंद्र द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति भी केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव का कारण बन जाती है।
प्रश्न 5.
सरकारिया आयोग पर एक नोट लिखें।
उत्तर:
सन् 1983 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने केंद्र-राज्यों के सम्बन्धों पर विचार करने के लिए एक तीन-सदस्यीय आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति आर०एस० सरकारिया को इस आयोग का अध्यक्ष तथा पी० शिवरामन और एस०आर० सेन को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 27 अक्तूबर, 1987 को पेश की। इस आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं
(1) आयोग ने राज्य सरकारों के वित्तीय साधन बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया है,
(2) आयोग ने राज्यों के अधिकार बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव दिए हैं। एक सुझाव यह है कि संविधान में संशोधन करके राज्यों को अनुच्छेद 242 के अन्तर्गत राज्य सूची के कानूनों में संशोधन करने का अधिकार दिया जाए,
(3) आयोग ने केंद्र व राज्य के विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद् गठित किए जाने की सिफारिश की है। प्रधानमन्त्री, केंद्रीय मन्त्रियों और सभी मुख्यमन्त्रियों को इस परिषद् में रखा जाए,
(4) आयोग के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति से पहले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री से परामर्श किया जाना चाहिए,
(5) राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति में विलम्ब रोका जाना चाहिए,
(6) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब रोका जाना चाहिए,
(7) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण उनकी स्वीकृति से किया जाना चाहिए,
(8) आयोग ने संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत विषयों पर कानून बनाने के सम्बन्ध में संयम बरतने की सलाह दी है,
(9) आयोग ने राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय योजनाएँ बनाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है,
(10) आयोग ने सुझाव दिया है कि स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव कराने और इनके समुचित कामकाज का संसद द्वारा कानून बनाना चाहिए,
(11) समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र द्वारा राज्यों से परामर्श अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए दृढ़ परम्परा का पालन किया जाए,
(12) आयोग ने कहा है कि सामान्य तौर पर केंद्र को केवल उन क्षेत्रों में कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें राष्ट्र के व्यापक हित में एक-सी नीति और कार्रवाई जरूरी है,
(13) आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद्, नीति आयोग जैसे संगठनों तथा अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत बनाने के भी सुझाव दिए हैं,
(14) आयोग की राय में राज्यों की क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था असफल रही है और इसे फिर सक्रिय किया जाना चाहिए,
(15) आयोग ने देश की एकता और अखण्डता के हित में सभी राज्यों में समान रूप से त्रि-भाषा फार्मूले को इसकी सही भावना से लागू करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की सिफारिश की है,
(16) राजभाषा के रूप में हिन्दी को सरल बनाने पर जोर देते हुए आयोग ने कहा है कि आसानी से समझे जाने वाले शब्दों के स्थान पर कठिन सांस्कृतिक शब्दों का उपयोग उचित नहीं है,
(17) आयोग ने कहा है कि राजभाषा के विकास के लिए यदि अंग्रेज़ी सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के उन प्रचलित शब्दों और रूप को, जो अब हिन्दुस्तान के हिस्से बन चुके हैं, निकाला गया तो वह संविधान के अनुच्छेद की भावना के विरुद्ध होगा।
आयोग के अनुसार संविधान के अन्तर्गत केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के वितरण में राज्यों की स्वतन्त्रता की आवश्यकताओं के साथ एक मजबूत केंद्र की जरूरत को महत्त्व दिया गया है। सरकारिया आयोग की सभी सिफारिशें केंद्रीय सरकार के विचाराधीन हैं और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रश्न 6.
राज्य की स्वायत्तता का क्या अर्थ है? इसकी माँग के मुख्य कारणों का वर्णन करें।
उत्तर:
भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन प्रारम्भ से ही विवादपूर्ण रहा है। संविधान सभा में भी अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई थी कि शक्ति विभाजन की यह योजना भारत संघ के घटक राज्यों को ‘नगरपालिकाओं’ का रूप देती है। वास्तविकता भी यही है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं और राज्य नामक इकाइयों को निश्चित रूप से कमजोर रखा गया है।
सन् 1967 तक राज्यों में तथा केंद्र में एक ही दल काँग्रेस की सरकार सत्ता में रहने से केंद्र राज्यों के बीच विवाद नहीं उठे, किन्तु सन् 1967 के बाद जब देश के 8 राज्यों में दूसरे दलों की गैर-काँग्रेसी सरकारें बनी तो केंद्र-राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण और सामंजस्य की समस्या पैदा हो गई। राज्यों की ओर से स्वायत्तता की माँग उठी।
राज्यों की स्वायत्तता की माँग के समर्थक यह मानते हैं कि संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करते हैं। यहाँ हम राज्यों की स्वायत्तता से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों; जैसे राज्य की स्वायत्तता की माँग के कारण एवं स्वायत्तता के पक्ष एवं विपक्ष में विभिन्न तर्कों का उल्लेख करेंगे।
राज्य की स्वायत्तता का अर्थ साधारण शब्दों में स्वायत्तता का अर्थ है कि किसी को भी अपने क्षेत्र में निर्बाध कार्य करने की स्वतन्त्रता अर्थात् आन्तरिक व बाह्य कार्य-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न होना। राज्यों के मामले में स्वायत्तता का अर्थ थोड़ा-सा भिन्न है। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ स्वतन्त्रता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्यों को उनके मामलों में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
राज्यों को शक्तियाँ संविधान द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और उन्हें उनका प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्यों को जन-कल्याण की योजनाएँ बनाने एवं उन्हें लागू करने की शक्तियाँ बिना किसी रोक-टोक के प्राप्त होनी चाहिएँ। यही नहीं वित्तीय क्षेत्र में भी राज्य स्वतन्त्र होने चाहिएँ। तभी राज्य की स्वायत्तता को लागू किया जा सकता है।
दूसरे शब्दों में, केंद्र का राजनीतिक व प्रशासनिक मामलों में न्यूनतम हस्ताक्षेप होना चाहिए। केंद्र का कार्य-क्षेत्र सीमित होना चाहिए। उसे केवल विदेश सम्बन्ध, रक्षा, मुद्रा और जन-संचार के विषयों के मामलों में शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिएँ। कराधान के क्षेत्र में भी उनकी शक्तियाँ सीमित होनी चाहिएँ। उन्हें केवल उतने ही कर लगाने का अधिकार दिया ।
जाना चाहिए, जितने उन्हें उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने के लिए आवश्यक हों। राज्यों को कराधान के इतने अधिकार प्रदान किए जाने चाहिएँ, जिससे कि वे साधनों का अभाव महसूस न करें। अतः राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ न तो राज्यों की स्वतन्त्रता से है और न ही प्रभुसत्ता से। यह एक ऐसा वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को कुछ क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता तथा कम-से-कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त हो एक निश्चित क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य के अधिकार का नाम ही राज्यों की स्वायत्तता है।
राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारण (Causes of demand for State Autonomy) भारत में राज्यों पर केंद्र के नियन्त्रण के अनेक साधन हैं। इन साधनों के कारण ही राज्यों की स्वायत्तता की माँग ने जन्म लिया। उन कारणों का विवरण निम्नलिखित है
1. संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा अवश्य किया गया है, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में दिए गए हैं (1) यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है।
संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाए तो संसद उस पर कानून बना सकती है, (2) राष्ट्रपति द्वारा आपात्काल की घोषणा हो जाने पर संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून बना सकती है। केंद्रीय संसद की शक्ति की व्यापकता का तीन बातों से पता चलता है-प्रथम, यदि समवर्ती सूची में तथा उन दोनों में कोई विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। द्वितीय, अवशिष्ट
शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हैं। तृतीय, यदि राज्य विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक का सम्बन्ध किसी निजी सम्पत्ति पर कब्जा करने अथवा उच्च न्यायालयों की शक्तियों को कम करने से हो तो राज्यपाल के लिए यह जरूरी है कि उस विधेयक को वह राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजे। अतः राज्य प्रशासन में केंद्र के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण ही राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की माँग जोर पकड़ रही है।
2. वित्तीय दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों को केंद्र का मुँह ताकना पड़ता है। केंद्र पर राज्यों की आर्थिक निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
3. अखिल भारतीय सेवाएँ तथा राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएँ जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) तथा भारतीय . पुलिस सेवा (I.P.S.) पर भारत की संघीय सरकार का नियन्त्रण है। इन सेवाओं से सम्बन्धित उच्च अधिकारी राज्यों में अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं। अतएव इन अधिकारियों के माध्यम से ही केंद्रीय सरकार राज्यों की सरकारों पर नियन्त्रण रखती है। जहाँ तक राज्यपाल का प्रश्न है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह राज्य में केंद्र के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है। .
4. राज्यों के बीच भाषायी एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भारत में राज्यों की भाषायी एवं सांस्कृतिक विभिन्नता भी राज्यों की स्वायत्तता की माँग को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा है। इसी आधार पर कुछ राज्य यह महसूस करते हैं कि हिन्दी भाषी राज्य गैर-हिन्दी भाषी राज्यों पर अपना आधिपत्य एवं प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी भावना से ग्रस्त होकर सन् 1960 के दशक में हिन्दी भाषा के विरोध में गैर-हिन्दी भाषायी राज्यों के द्वारा आन्दोलन चलाए गए। अतः ऐसी माँग एवं भावनाएँ ही भारतीय संघवाद के स्वरूप को चुनौती देने के साथ-साथ राज्यों की स्वायत्तता की माँग के रूप में आगे बढ़ती जा रही हैं।
5. राज्यपाल की भूमिका एवं राष्ट्रपति शासन-अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे संघों में केंद्र को यह शक्ति प्रदान नहीं है कि राज्यों की स्वायत्तता (Autonomy) समाप्त कर सके, किंतु भारत में आपात्काल की घोषणा किए जाने पर संविधान एकात्मक रूप धारण कर लेता है। आपात्काल में केंद्रीय संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में सम्मिलित हैं।
जब राष्ट्रपति यह घोषणा कर देता है कि किसी राज्य की सरकार संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाई जा रही, तो राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाती है और राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल को राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य का राज्यपाल जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। राज्यपाल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
इसलिए राज्यपाल केवल मात्र राज्यों में केंद्र सरकार का एजेण्ट बनकर कार्य करता है। केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर विशेषतः विपक्षी दलों की सरकार को भंग करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार राज्यपाल के पद के माध्यम से राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है।
इसी कारण आज राज्यपाल का पद सबसे अधिक विवादित पद बना हुआ है। राज्यों में राज्यपाल के निर्णयों एवं केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर, न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग गलत ढंग से किया जाता रहा है।
इसीलिए केंद्र राज्य सम्बन्धों सम्बन्धी गठित सरकारिया आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति दी थी कि राज्यपाल के पद पर गैर-राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए ताकि यह संविधान के अनुसार बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के निष्पक्ष होकर अपना कार्य कर सके, परन्तु अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है। इसीलिए राज्यों के द्वारा निरन्तर स्वायत्तता की माँग जोर पकड़ती जा रही है।
6. अन्तर्राज्यीय झगड़े-राज्यों के बीच भाषायी एवं सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ-साथ राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी एवं नदी जल सम्बन्धी विवादों का केंद्र सरकार द्वारा समुचित समाधान न करवाने के कारण भी राज्यों की स्वायत्तता की माँग को बल दिया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड एवं पंजाब व हरियाणा के बीच राजधानी चण्डीगढ़ को लेकर आज भी विवाद कायम है।
इसी तरह से तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद एवं गुजरात, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी जल-विवाद आदि ने राज्यों के बीच संघात्मक भावना को जहाँ ठेस पहुंचाई है, वहीं केंद्र के प्रभावी नियन्त्रण के अभाव ने भी राज्यों की स्वायत्तता की माँग को बल देने का कार्य किया है।
7. संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सकती है –अमेरिका . या ऑस्ट्रेलियाई संघ व्यवस्था में केंद्र राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उनकी सीमाओं में हेर-फेर नहीं कर सकता, परन्तु भारत में केंद्रीय संसद नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों के आकार को घटा या बढ़ा सकती है। ऐसा करने के लिए संसद को राज्यों की अनुमति नहीं लेनी पड़ती।
8. राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं विश्व की अधिकांश संघ व्यवस्थाओं में संसद के उच्च सदन का संगठन राज्यों की समानता के सिद्धान्त के आधार पर किया गया है। समानता का सिद्धान्त इसलिए अपनाया गया है जिससे केंद्रीय संसद पर बड़े राज्य का आधिपत्य कायम न हो सके, परन्तु भारत के उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा में सभी राज्यों का बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं होता।
9. राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं-अमेरिका और स्विट्जरलैंड के राज्यों के अपने पृथक् संविधान हैं और उनमें संशोधन करने की शक्तियाँ भी राज्यों के विधानमण्डलों को ही प्राप्त हैं, परन्तु भारत में एक ही संविधान है जो केंद्र और राज्यों दोनों की संरचना और शक्तियों का उल्लेख करता है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे भारतीय संविधान की उन धाराओं में संशोधन कर सकें जिनका उनकी संरचना और प्रकार्यों से सम्बन्ध है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत केवल संसद ही कर सकती है।
निष्कर्ष दिए गए कारणों की वजह से विभिन्न राज्यों में राज्य की स्वायत्तता की माँग ने जोर पकड़ा। डी०एम०के० तथा : अन्ना डी०एम०के० ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता की माँग की। मार्क्सवादी दल ने संविधान की प्रस्तावना से ‘यूनियन’ शब्द को हटाकर ‘फेडरल’ शब्द का उल्लेख करने की माँग की। इसी प्रकार अकाली दल ने पंजाब में राज्य की स्वायत्तता के लिए उग्र आन्दोलन चलाया। जम्मू और कश्मीर में भी इसी प्रकार की माँग को लेकर कई सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
प्रश्न 7.
राज्यों की स्वायत्तता के विभिन्न प्रश्नों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
राज्यों की स्वायत्तता के विभिन्न प्रश्न (Various Issues of State Autonomy)-राज्यों की स्वायत्तता का मामला एक अहम् एवं कठिन विषय है जिसके चलते देश की एकता पर संकट आ सकता है। समय-समय पर राज्यों की स्वायत्तता से सम्बन्धित जिन मामलों पर आवाज उठाई गई वे विषय इस प्रकार हैं
1. राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का है। वह राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमन्त्री के परामर्श से करता है। साधारणतया राज्यपाल की नियुक्ति में अमुक राज्य के मुख्यमन्त्री की सलाह नहीं ली जाती। विपक्षी दलों की यह माँग रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्यमन्त्री की सलाह ली जानी चाहिए।
केंद्र द्वारा अनेकों बार राज्य की सलाह लिए बिना राज्यपाल की नियुक्ति की है जिसका राज्य सरकार द्वारा विरोध किया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार और राज्यपाल के सम्बन्धों में खटास पैदा हो जाती है। यही नहीं जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है तो जिन राज्यों में विपक्ष सत्ता में होता है तो राज्यपालों के इस्तीफे माँग लिए जाते हैं।
जैसा 2004 में काँग्रेस के सत्ता में आने के बाद, एन०डी०ए० (N.D.A.) द्वारा नियुक्त राज्यपालों के इस्तीफे माँग लिए गए। इस विवाद को लेकर अन्तर्राज्यीय परिषद् में कई बार चर्चा हुई और यह सुझाव दिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति में सम्बन्धित राज्य से सलाह लेने की प्रक्रिया को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।
2. राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन-राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है और वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर ऐसे कार्य कर देता है जो उसे नहीं वह राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज देता है जिसके स्वीकार होते ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।
इस मामले में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही है। राज्यपाल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता। अभी तक अनेकों उदाहरण हैं जबकि राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सन् 1952 से अब तक लगभग 130 बार से भी अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। इन मामलों में राज्यपाल की भूमिका निन्दा का पात्र बनी। सन् 2005 में बिहार में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया जिसकी विपक्ष ने जमकर आलोचना की। ऐसे में राज्यों की स्वायत्तता माँगना स्वाभाविक है।
3. राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में देरी-राज्यों को यह शिकायत रहती है कि जिन विधेयकों को विधानमण्डल पारित कर देती है, उन पर स्वीकृति देने में केंद्र अनावश्यक देरी करता है। कुछ पर स्वीकृति नहीं दी जाती और इसकी सूचना तक भी राज्य सरकार को नहीं दी जाती। कुछ पर भेदभाव की नीति अपनाई जाती है। माँग होने पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति की अवधि निश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाता। इस प्रकार राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने में देरी होना भी राज्यों की स्वायत्तता की माँग बढ़ाता है।
4. अखिल भारतीय सेवाओं का पक्षपातपूर्ण प्रयोग-अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र द्वारा नियन्त्रित और अनुशासित हैं। इन सेवाओं के किसी सदस्य का व्यवहार सेवा की शर्तों, आचार संहिता आदि के कितना ही विरुद्ध, आपत्तिजनक एवं पक्षपातपूर्ण क्यों न हो राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति के बिना इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती।
इससे राज्य सरकारें शिथिल होती हैं। कई बार तो केंद्र से प्रोत्साहन पाकर इन सेवाओं के सदस्य राज्य सरकारों की योग्यता, कुशलता पर ही प्रश्न-चिह्न लगा देते हैं। केंद्र में जब सत्ताधारी पार्टी इन सेवाओं का प्रयोग विपक्षी राज्य सरकारों को बदनाम करने के लिए करती है और सेवा के उन सदस्यों को पदोन्नत कर पुरस्कृत करती है जो राज्य सरकारों की उपेक्षा कर केंद्र के आदेशों का सीधे पालन करते हैं तो राज्यों में बेचैनी पैदा होती है।
इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं का पक्षपातपूर्ण प्रयोग, केंद्र एवं राज्यों के सम्बन्धों में दरार पैदा करता है। अतः स्पष्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के पक्षपातपूर्ण ढंग के प्रयोग ने राज्यों की स्वायत्तता की माँग को बढ़ावा दिया है।
5. केंद्र का राज्यों की विपक्षी सरकारों एवं उनकी समस्याओं के प्रति असवेदनशील एवं उदासीन व्यवहार केंद्र का दृष्टिकोण राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों के प्रति असंवेदनशील और उदासीन रहा है। केंद्र एक लम्बे समय तक समस्याओं पर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, जो अन्ततः केंद्र और राज्यों में टकराव पैदा करती हैं।
विपक्षी दल की राज्य सरकारों के प्रति असंवेदनशीलता का एक अन्य पहलू दो राज्य सरकारों के परस्पर विवाद में उस राज्य सरकार की समस्या के प्रति उदासीन हो जाना भी देखने में आया, जो दूसरे दल की थी। जनवरी, 1994 में पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली की सरकार के विवाद को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अन्तर्गत हरियाणा के मुख्यमन्त्री ने दिल्ली को होने वाली पानी की सप्लाई को कम कर दिया, चूंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार थी।
इस पर केंद्र सरकार चुप बनी रही और उस पर भी तभी जूं रेंगी जब दिल्ली सरकार ने केंद्रीय मन्त्रियों की पानी की सप्लाई को रोकने की चेतावनी दी। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि केंद्र-राज्य, सम्बन्ध में केंद्र सरकार की नीति प्रारम्भ से ही राज्यों को अपने ऊपर आश्रित बनाए रखने की रही है। सन् 1967 से राज्यों में केंद्र के हस्तक्षेप की यह नीति खुलकर सामने आई जो कि सन् 1995 तक जारी रही।
सन् 1996 से केंद्र में मिली-जुली सरकारों में क्षेत्रीय दलों के प्रभावी होने के कारण यह प्रवृत्ति कमजोर हो रही है और आम-सहमति की नीति का विकास हो रहा है। अतः कहा जा सकता है कि केंद्र के राज्यों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार ने राज्यों की स्वायत्तता की माँग को न केवल जन्म दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया है।
6. राज्यों की वित्तीय दुर्दशा-राज्यों की वित्तीय स्थिति में निरन्तर गिरावट ने नीति निर्धारकों के सामने जटिल समस्याएँ खड़ी कर दी हैं जिनके कारण राज्यों में न तो विकास गति पकड़ रहा है और न ही पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। राजस्व में निरन्तर कमी, वित्तीय और प्राथमिक घाटे, कों के बढ़ते बोझ और अन्य देनदारियाँ, पूँजीगत खाते और रख-रखाव के खर्चों में कमी इत्यादि राज्यों की वित्तीय दुर्दशा के संकेत हैं।
साथ ही राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता की वृद्धि का संकुचन और केंद्रीय वेतन पुनः निरीक्षण के प्रभाव ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर घातक प्रभाव डाला है। ऐसी स्थिति के लिए केंद्र की अपेक्षा राज्य सरकारें स्वयं ही अधिक जिम्मेदार हैं। अतः राज्यों की स्वायत्तता के लिए राज्यों की वित्तीय दुर्दशा भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
7. दूरदर्शन और आकाशवाणी का पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल केंद्र का दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे महत्त्वपूर्ण जन-संचार साधनों पर पूर्ण नियन्त्रण और एकाधिकार है। सन् 1966 में चन्दा समिति ने इन्हें स्वायत्तशासी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया। दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा बन गया है जिसने केंद्र और राज्यों के बीच उत्तेजना पैदा की है।
राज्यों की जन-संचार के इन साधनों के विरुद्ध ये शिकायतें रहीं-
(1) खबरें निष्पक्ष भाव से एवं पक्षपातरहित होकर प्रसारित नहीं की जातीं। यह स्थिति अत्यधिक उत्तेजना उस समय पैदा करती है जब किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र और विपक्षी राज्य सरकारों में नीति सम्बन्धी कोई महत्त्वपूर्ण मतभेद होता है और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी राज्यों के दृष्टिकोण की उपेक्षा करके केवल केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं।
(2) राज्यों को विशेषकर चुनाव के समय प्रचार सुविधाएँ नहीं दी जातीं।
(3) देश के विविध जातीय एवं सांस्कृतिक समूहों को समुचित प्रतिनिधित्व न देना। इस प्रकार केंद्र द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी को पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल करना, राज्यों के लिए द्वितीय या अतिरिक्त चैनल खोलने की माँग को जन्म देती है। अतः इस प्रकार दूरदर्शन और आकाशवाणी का पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रयोग राज्यों की स्वायत्तता के लिए एक मुद्दा है।
8. समवर्ती सूची-राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद के द्वारा कानून बनाने की स्थिति में राज्यों द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होता। इसलिए विपक्षी दल समवर्ती सूची को पूर्णरूपेण राज्यों के अधीन करने के पक्ष में हैं।
9. अवशिष्ट शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियों को लेकर भी केंद्र व राज्यों में तनाव है। यह भी राज्यों की स्वायत्तता की माँग को बढ़ावा देने का कारण है। राज्य सभी अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के देने के पक्ष में है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें
1. संविधान द्वारा भारत को कहा गया है
(A) संघीय राज्य
(B) एकात्मक राज्य
(C) राज्यों का संघ
(D) बनावट में संघात्मक, परंतु भाव में एकात्मक
उत्तर:
(C) राज्यों का संघ
2. संविधान में संघीय सूची में मूलतः विषयों की संख्या कितनी है?
(A) 97
(B) 99
(C) 100
(D) 102
उत्तर:
(A)97
3. संघीय सूची में दिए गए विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है
(A) संसद के पास
(B) राज्यसभा के पास
(C) लोकसभा के पास
(D) राज्य विधानमंडल के पास
उत्तर:
(A) संसद के पास
4. संविधान में राज्य-सूची में मूलतः कुल विषय कितने दिए गए हैं?
(A) 97
(B) 61
(C) 66
(D) 47
उत्तर:
(C) 66

5. संविधान में समवर्ती सूची में मूलतः कुल विषय कितने दिए गए हैं?
(A) 61
(B) 47
(C) 52
(D) 66
उत्तर:
(B) 47
6. समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के संबंध में कानून पास करने का अधिकार है
(A) संसद के पास
(B) राज्य विधानमंडलों के पास
(C) संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के पास
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के पास
7. समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय के संबंध में संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा परस्पर विरोधी कानून बनाने की स्थिति में
(A) दोनों कानून रद्द हो जाएँगे
(B) संसद द्वारा पास किया गया कानन लाग होगा
(C) राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया गया कानून लागू होगा
(D) दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा
उत्तर:
(B) संसद द्वारा पास किया गया कानून लागू होगा
8. भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं?
(A) 26
(B) 21
(C) 28
(D) 29
उत्तर:
(C) 28
9. निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद राज्य-सूची में दिए गए विषयों के संबंध में भी कानून बना सकती है
(A) संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने पर
(B) दो अथवा दो से अधिक राज्यों द्वारा ऐसी प्रार्थना करने पर
(C) किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए
(D) उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में
10. वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार निम्नलिखित को है
(A) राष्ट्रपति
(B) उप-राष्ट्रपति
(C) संसद
(D) प्रधानमंत्री
उत्तर:
(A) राष्ट्रपति
11. अंतर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) की स्थापना करने का अधिकार निम्नलिखित को प्राप्त है
(A) राज्यपाल
(B) राष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) मुख्य न्यायाधीश
उत्तर:
(B) राष्ट्रपति
12. भारत की संघीय व्यवस्था का संरक्षक है
(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) प्रधानमंत्री
(D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर:
(D) सर्वोच्च न्यायालय
13. भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है?
(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) प्रधानमंत्री
(D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर:
(B) संसद
14. शिक्षा निम्नलिखित सूची का विषय है
(A) संघ सूची
(B) राज्य-सूची
(C) समवर्ती सूची
(D) अवशिष्ट शक्तियाँ
उत्तर:
(C) समवर्ती सूची
15. भारतीय संघ में कुल कितने संघीय क्षेत्र हैं?
(A) 7
(B) 10
(C) 9
(D) 8
उत्तर:
(D) 8
16. शेष शक्तियों (Residuary Powers) के संबंध में कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित को है
(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) राज्य विधानमंडल
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(B) संसद
17. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघीय सूची में है?
(A) विदेशी मामले
(B) विवाह और तलाक
(C) शिक्षा
(D) स्थानीय सरकार
उत्तर:
(A) विदेशी मामले
18. निम्नलिखित विषय राज्य-सूची में शामिल है
(A) प्रतिरक्षा
(B) डाक
(C) कृषि
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) कृषि
19. निम्नलिखित विषय समवर्ती-सूची में शामिल हैं
(A) विदेशी मामले
(B) शिक्षा
(C) कृषि
(D) पुलिस एवं जेलें
उत्तर:
(B) शिक्षा
20. वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है
(A) प्रधानमंत्री को
(B) राष्ट्रपति को
(C) संसद को
(D) लोकसभा को
उत्तर:
(B) राष्ट्रपति को
21. “भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है पर भावना में एकात्मक है।” यह किसने कहा?
(A) डी०एन० बनर्जी ने
(B) दुर्गादास बसु ने
(C) डॉ० अम्बेडकर ने
(D) के०सी० बीयर ने
उत्तर:
(A) डी०एन० बनर्जी ने
22. “भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण है।” यह कथन किसका है?
(A) डी०डी० बसु का
(B) के०सी० बीयर का
(C) जी०एन० जोशी का
(D) जी०एन० सिंह का
उत्तर:
(A) डी०डी० बसु का
23. 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़े गए विषयों से समवर्ती सूची के विषयों की कुल संख्या कितनी हो गई?
(A) 47
(B) 49
(C) 52
(D) 66
उत्तर:
(C) 52
24. वर्तमान में राज्यसूची में कितने विषय हैं?
(A) 47
(B) 52
(C) 66
(D) 61
उत्तर:
(D) 61
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें
1. भारतीय संविधान में संघ के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
उत्तर:
राज्यों का संघ (Union of States)।
2. शक्तियों के विभाजन की तीन सूचियों में मूलतः कितने-कितने विषय शामिल हैं?
उत्तर:
संघीय सूची में 97, राज्य-सूची में 66 तथा समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल हैं।
3. भारतीय संघ में कुल कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं?
उत्तर:
भारतीय संघ में कुल 28 राज्य एवं 8 संघीय क्षेत्र हैं।
4. भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है?
उत्तर:
भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है।
5. भारत में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कब हुई?
उत्तर:
भारत में अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना 28 मई, 1990 को हुई।
6. संविधान में शक्तियों के विभाजन के आधार पर कौन-सी शासन-प्रणाली अपनाई गई है?
उत्तर:
संविधान में शक्तियों के विभाजन के आधार पर संघात्मक शासन-प्रणाली अपनाई गई है।
7. भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं?
उत्तर:
भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय संसद को प्रदान की गई हैं।
8. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया?
उत्तर:
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त, 2019 को पारित हुआ।
9. नीति आयोग कब अस्तित्व में आया?
उत्तर:
1 जनवरी, 2015 को।
10. जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया?
उत्तर:
जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 5 एवं 6 अगस्त, 2019 को पारित हुआ।
रिक्त स्थान भरें
1. “भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है, परन्तु भाव में एकात्मक है।” यह कथन ……………. ने कहा।
उत्तर:
डी०एन० बनर्जी
2. अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ………….. को प्राप्त है।
उत्तर:
संसद
3. भारतीय संघ में …………… केंद्र शासित प्रदेश हैं।
उत्तर:
8
4. संघीय सूची में ……………. विषय हैं।
उत्तर:
97
5. राज्य सूची में …………… विषय हैं।
उत्तर:
61
6. शिक्षा ……………. सूची का विषय है।
उत्तर:
समवर्ती
7. भारत में वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार को है।
उत्तर:
राष्ट्रपति
8. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ………………….हैं।
उत्तर:
राजीव कुमार
![]()
![]()
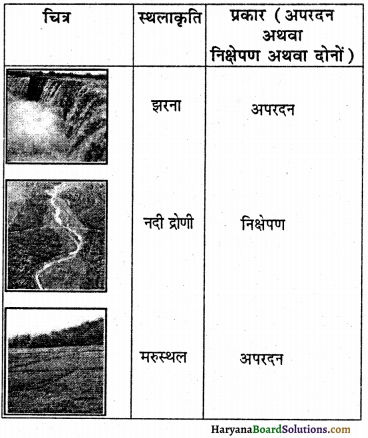
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()