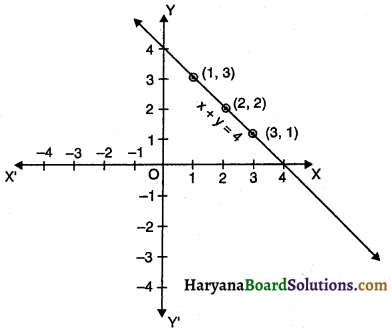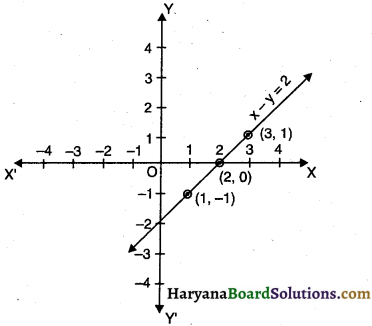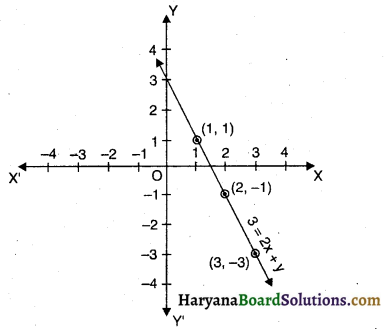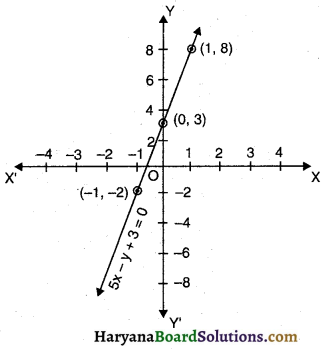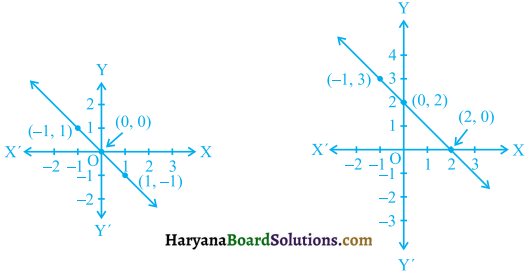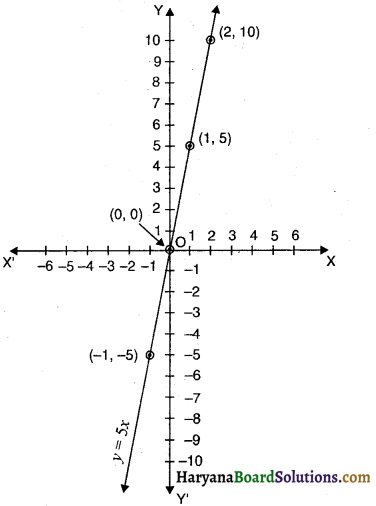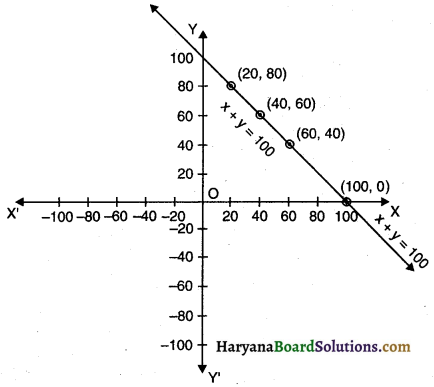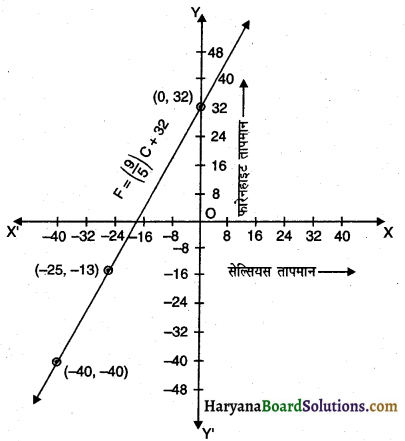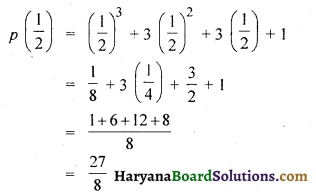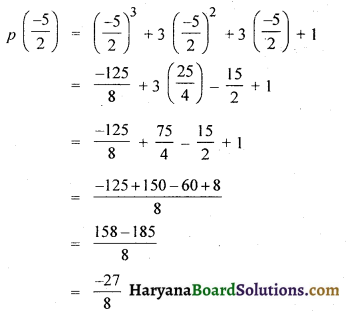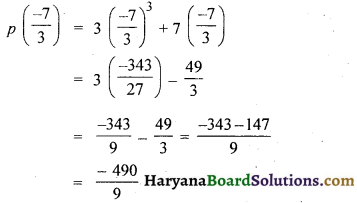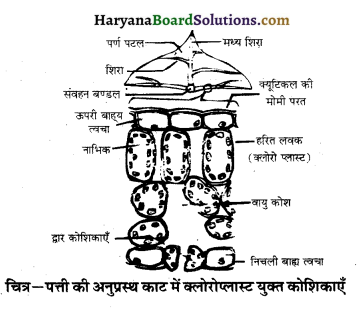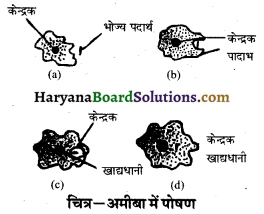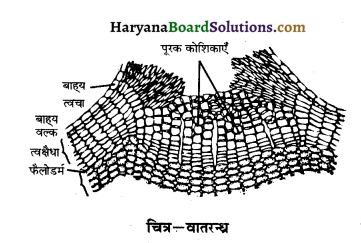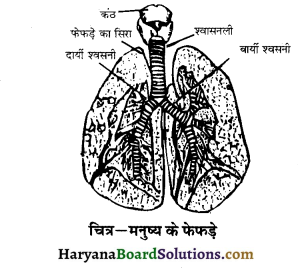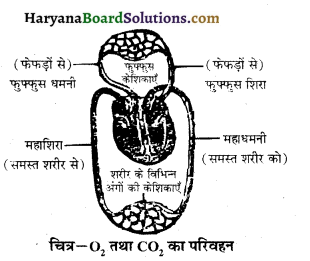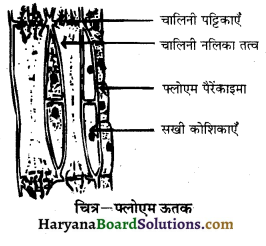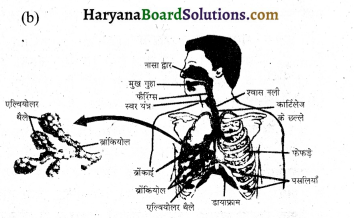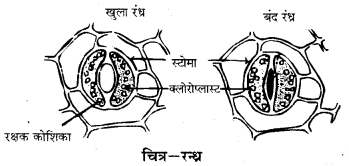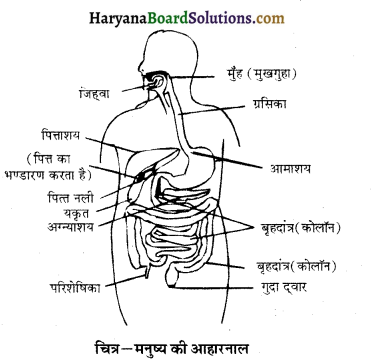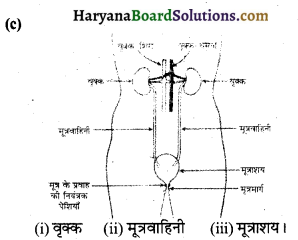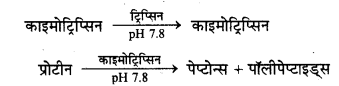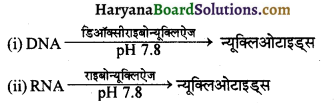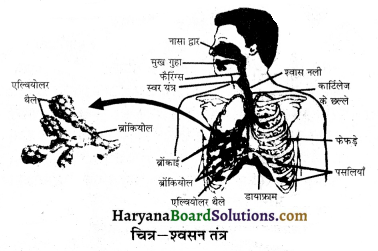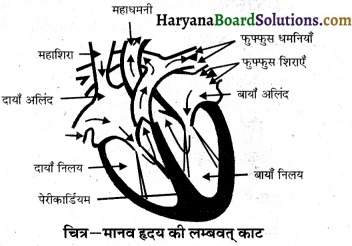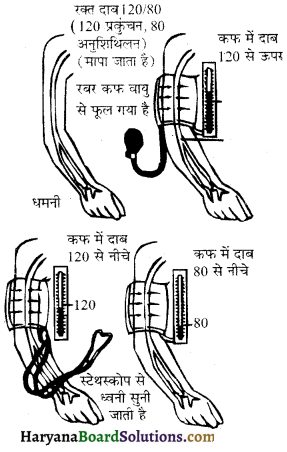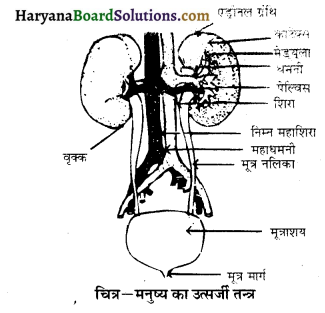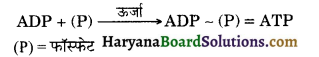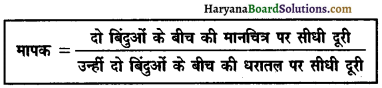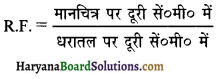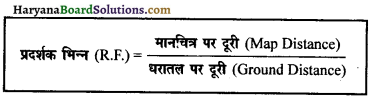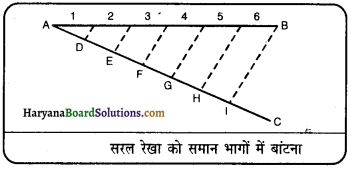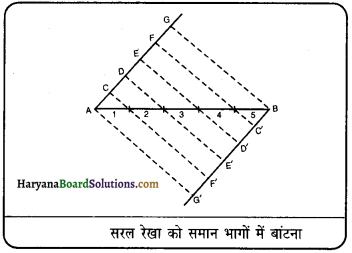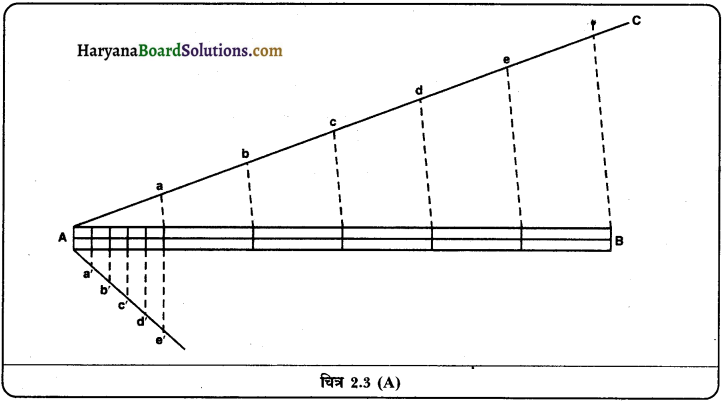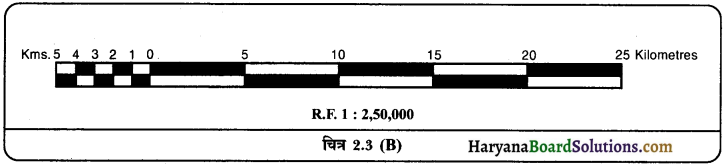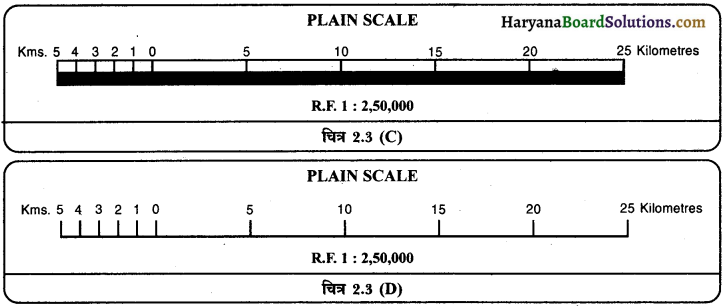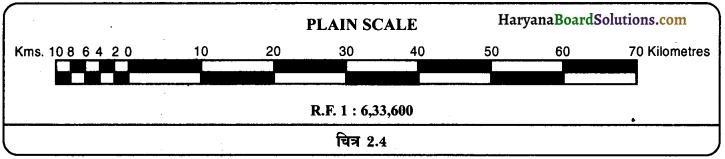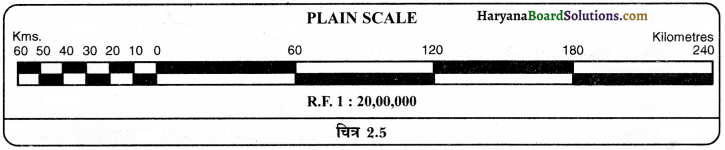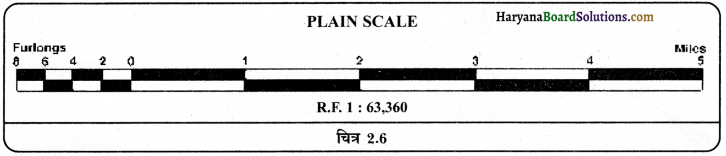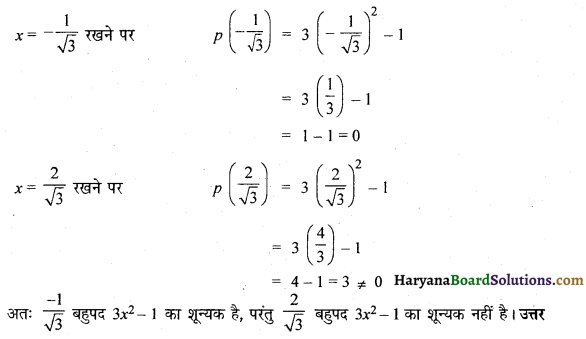Haryana State Board HBSE 12th Class Political Science Important Questions Chapter 1 शीतयुद्ध का दौर Important Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Political Science Important Questions Chapter 1 शीतयुद्ध का दौर
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
शीतयुद्ध क्या है ?
द्वितीय विश्व-युद्ध वह घटना थी जिसने विरोधी विचारधारा में विश्वास रखने वाले राज्यों रूस तथा अमेरिका को एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर बाध्य कर दिया था। रूस ने अपने विरोधी राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राज्यों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लडाई लडी।
रूस और पश्चिमी राज्यों के इस युद्धकालीन सहयोग को देखते हुए यह आशा की जाने लगी थी कि युद्ध के बाद विश्व में अवश्य ही स्थायी शान्ति की स्थापना की जाएगी। युद्ध काल के यह मित्र शान्तिकाल की समस्याओं का समाधान भी मिलजुल कर निकालेंगे तथा विश्व में शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में भी सहयोग करेंगे। परन्तु युद्धकालीन सहयोग तथा मित्रता शान्तिकालीन बोझ सहन न कर सकी और मित्रता का यह रेत का महल एकदम ढह गया।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों राज्यों के सम्बन्धों में आश्चर्यजनक मोड़ आया। इनके सम्बन्ध तनावपूर्ण होते चले गए। युद्ध काल के साथी युद्ध के बाद एक-दूसरे के लिए अजनबी बन गए। इतना ही नहीं वे एक-दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए। आज तक दोनों के सम्बन्ध उसी प्रकार शत्रुता, कटुता तथा वैमनस्य से परिपूर्ण चले आ रहे हैं। इन्हीं सम्बन्धों की व्याख्या के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है।
शीतयुद्ध को विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है। के० पी० एस० मैनन के शब्दों में, “शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह पराकाष्ठा पर था दो व्यक्तियों के मध्य दृढ़ संघर्ष था।
विचारधारा भी पूंजीवादी तथा साम्यवादी, पद्धतियां भी संसदीय जनतन्त्र तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, गुट के नाटो तथा वार्सा पैकट, राज्य के संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ तथा व्यक्ति के जोसफ स्टालिन तथा जॉन फास्टर डलेस।” इसी प्रकार एक अन्य लेखक के शब्दों में, “शीत युद्ध ने वास्तव में 1945 के बाद के समय में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जो न शान्ति का था न युद्ध का, इसने पूर्व पश्चिम के विभाजन अविश्वास, शंका तथा शत्रुता को अपरत्व प्रदान कर दिया था।”
पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह दिमागों में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध है। नोर्थेज ग्रीब्ज के शब्दों में, “हमने देखा है कि किस प्रकार 1945 में प्रमुख धुरी राष्ट्रों जर्मनी तथा जापान की पराजय के बाद 15 वर्षों तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर दो महाशक्तियों अमेरिका तथा रूस की निरन्तर विरोधता का प्रभुत्व रहा। इसमें उनके साथी परन्तु अधीनस्थ राज्य भी लिप्त थे। इस स्थिति को वाल्टर लिपमैन के द्वारा शीतयुद्ध कहकर पुकारा गया जिसकी विशेषता दो गुटों में उग्र शत्रुता थी।”
इसी प्रकार फ्लोरैंस एलेट तथा मिखाईल समरस्किल ने अपनी पुस्तक ‘A Dictionary of Politics’ में शीतयुद्ध को राज्यों में तनाव की वह स्थिति जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा दूसरे को निर्बल बनाने की वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त नीतियां अपनाता है, बताया है।
डॉ० एम० एस० राजन (Dr. M.S. Rajan) के अनुसार, “शीतयुद्ध शक्ति-संघर्ष की राजनीति का मिला-जुला परिणाम दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिन्तन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक-दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है।”
पं० जवाहर लाल नेहरू (Pt. Jawahar Lal Nehru) के अनुसार, “शीतयुद्ध पुरातन शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा का नया रूप है, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर, दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है।”
जॉन फॉस्टर डलेस (John Foster Dales) के अनुसार, “शीतयुद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था, अच्छाई का बुराई के विरुद्ध, सही का ग़लत के विरुद्ध एवं धर्म का नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था।”
लुईस हाले (Louis Halle) के अनुसार, “शीतयुद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है, जो शस्त्र-युद्ध से एकदम भिन्न किन्तु इससे अधिक भयानक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने की अपेक्षा उन्हें और उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर या कोरिया हो अथवा अरब-इज़रायल संघर्ष हो-सभी शीतयुद्ध में मोहरों की तरह प्रयोग किए गए।”
इस प्रकार शीतयुद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका तथा रूस अथवा दो गुटों के बीच व्याप्त उन कटु सम्बन्धों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित है। इसके अन्तर्गत दोनों गुट एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबन्धन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार सैनिक हस्तक्षेप अधिकाधिक शस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा लेते हैं। –
शीत युद्ध की विशेषताएँ
(1) शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति भी है जिसे मूलत: ‘गर्म शान्ति’ कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शान्ति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध’ होता है, बल्कि शान्ति एवं युद्ध के मध्य की अस्थिर स्थिति बनी रहती है।
(2) शीत युद्ध, युद्ध का त्याग नहीं, अपितु केवल दो महाशक्तियों के प्रत्यक्ष टकराव की अनुपस्थिति माना जाएगा।
(3) यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, किन्तु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है।
(4) शीत युद्ध एक वाक्युद्ध था जिसके अन्तर्गत दो पक्ष एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे जिसके कारण छोटे-बड़े सभी राष्ट्र आशंकित रहते हैं।

प्रश्न 2.
पश्चिमी गुट के अनुसार रूस किस प्रकार शीतयुद्ध के लिए ज़िम्मेदार था ?
अथवा
शीतयुद्ध उत्पन्न होने के मूलभूत कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
8 मई, 1945 को यूरोप में युद्ध का अन्त हुआ। 25 अप्रैल, 1945 को रूस तथा अमेरिका की सेनाओं का यूरोप के मध्य आमना-सामना हो गया। दोनों सेनाएं ऐलबे (Elbe) नदी के किनारों पर खड़ी हो गई थीं तथा यही समकालिक इतिहास की वह प्रमुख अवस्था थी जो कभी नहीं बदली, इस प्रमुख अवस्था का कारण कोई अणु बम्ब या साम्यवाद नहीं था।
इसका कारण था जर्मनी तथा अन्य यूरोपियन राज्यों का रूस तथा अमेरिका में बंटवारा। इस विभाजन के कारण ही शीत युद्ध का प्रारम्भ हुआ। यह तो मात्र एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस स्थिति तक पहुंचने के पीछे वास्तव में कई मुख्य कारण थे। शीतयुद्ध के लिए पूर्व तथा पश्चिम दोनों एक-दूसरे को उत्तरदायी ठहराते हैं। दोनों ही को एक दूसरे के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं जिनको एक-दूसरे के अनुसार शीतयुद्ध के कारण कहा जाता है।
पश्चिमी गुट के अनुसार रूस का उत्तरदायित्व (Responsibility of Russia according to Western Block)-पश्चिमी राष्ट्र शीत युद्ध के लिए निम्न कारणों से रूस को उत्तरदायी समझते हैं–
1. विचारधारा सम्बन्धित कारण (Ideological Reason):
पश्चिमी विचारधारा के अनुसार साम्यवाद के सिद्धान्त तथा व्यवहार में इसके जन्म से ही शीत युद्ध के कीटाणु भरे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर रूस द्वितीय विजेता के रूप में प्रकट हुआ था तथा यह द्वितीय महान् शक्ति था। अमेरिका तथा रूस वास्तव में दो ऐसी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कभी तालमेल नहीं हो सकता तथा जो पूर्णतया एक-दूसरे की विरोधी पद्धतियां हैं।
अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश पूंजीवादी लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं तथा रूस साम्यवाद में, यह कहा जा सकता है कि शीतयुद्ध तो उसी समय आरम्भ हो गया था जब 1918 में रूस में क्रान्ति हुई थी तथा उसके परिणामस्वरूप वहां साम्यवादी पद्धति की स्थापना हुई थी, पश्चिमी राष्ट्रों ने तभी से रूस को सन्देह की दृष्टि से देखना आरम्भ कर दिया था। उन्होंने रूस की क्रान्ति को असफल बनाने के प्रयास भी किए। इससे रूस तथा पश्चिमी राज्यों में गहरी दरार उत्पन्न हो गई यही कारण था कि एक लम्बे समय तक रूस तथा पश्चिमी राज्य फासिज्म के विरुद्ध एक न हो सके।
यहां तक कि 1914 में जब तक जर्मनी ने रूस पर आक्रमण न कर दिया वह इस युद्ध को एक साम्राज्यवादी युद्ध मानता रहा। रूस पर जर्मनी के आक्रमण के बाद पश्चिमी राज्यों ने उससे मित्रता कर ली, पर सैद्धान्तिक मतभेद यूं का यूं मौजूद रहा। इधर रूस ने भी अपने आप को विश्व साम्यवादी क्रान्ति को समर्पित कर दिया अर्थात् साम्यवादी विचारधारा में यह सिद्धान्त था कि वह बाकी के विश्व में भी साम्यवादी क्रान्ति को फैलाए।
रूस ने पहले पहल तो प्रकट तथा प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया कि इसका अर्थ था कि पश्चिमी राज्यों में पूंजीवादी तथा प्रजातान्त्रिक ढांचे को नष्ट करना जिसके बिना इस प्रकार की क्रान्ति सफल नहीं हो सकती थी। अतः जब तक रूस स्पष्ट रूप से विश्व साम्यवादी क्रान्ति को पाने के लक्ष्य को त्याग न दे तो पश्चिमी देशों के लिए उस पर सन्देह करना स्वाभाविक ही है क्योंकि इस प्रकार की क्रान्ति उनके लिए मृत्यु का प्रत्यक्ष सन्देश है।
2. रूस की विस्तारवादी नीति (Extentionist Policy of Russia):
शीतयुद्ध के लिए एक अन्य कारण के लिए भी पश्चिमी राज्य रूस को उत्तरदायी ठहराते हैं। उनका कहना है कि युद्ध के बाद भी रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखा। जार बादशाहों के काल में भी रूस पूर्वी यूरोप पर तथा विशेषकर बल्कान प्रायद्वीप के देशों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। रूस की इस साम्यवादी नीति को सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं।
एक तो स्टालिन याल्टा सम्मेलन में किए गए अपने वादों से मुकर गया तथा उसने पूर्वी यूरोप के देशों में निष्पक्ष चुनाव पान पर अपनी समर्थक सरकारें बना लीं। उसने ईरान से अपनी सेनाओं को न हटाया। तुर्की पर भी अनुचित दबाव डालने का प्रयास किया गया। इस प्रकार अमेरिका के मन में उसकी विस्तारवादी नीति के बारे सन्देह होता चला गया जिसको रोकने के लिए उसने भी कुछ कदम उठाए जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया।
3. रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना (Violation of Yalta agreement by Russia):
पश्चिमी राज्यों की रूस के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसने याल्टा सम्मेलन में किए गए अपने वादों का खुलेआम उल्लंघन किया। याल्टा सम्मेलन में निर्णय किया गया था कि पोलैण्ड में एक मिश्रित सरकार बनाई जाएगी तथा यह कहा गया कि उसमें फासिस्टों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। वहां पर फासिस्ट कौन हैं इस बात का निर्णय करने का अधिकार उस शक्ति को होगा जिसका वहां पर आधिपत्य होगा। रूस ने पोलैण्ड में लुबनिन सरकार की स्थापना कर रखी थी।
उसमें कुछ परिवर्तन करके लन्दन की प्रवासी सरकार के भी कुछ प्रतिनिधि ले लिए गए। परन्तु सभी महत्त्वपूर्ण विभाग कम्युनिस्ट मन्त्रियों के हाथों में थे। इतना ही नहीं वहां पर जिसने भी रूस का इस बात पर विरोध किया रूस ने उसे फासिस्ट करार कर गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार पोलैण्ड में कुछ समय के बाद पूर्णतया साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। पश्चिमी देशों ने इनका विरोध किया क्योंकि यह उनके अनुसार याल्टा समझौते का खुला उल्लंघन था।
पोलैण्ड के साथ-साथ याल्टा सम्मेलन में अन्य पूर्वी यूरोप के देशों के बारे में भी यही निर्णय किया गया था कि वहां पर निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव करवाए जाएंगे। रूस ने यह वचन दिया था कि वह उसकी सेनाओं के द्वारा स्वतन्त्र कराए गए राज्यों में चुनाव कराएगा। रूस के द्वारा चीन में भी याल्टा समझौते की अवहेलना की गई थी। मन्चूरिया में रूस की सेनाओं ने राष्ट्रवादी सेनाओं को घुसने नहीं दिया। इसके विपरीत साम्यवादी सेनाओं को न केवल घुसने ही दिया बल्कि उनको वह युद्ध सामग्री भी सौंप दी जो जापानी सेनाएं भागते समय छोड़ गई थीं इससे भी मित्र राष्ट्रों का क्षुब्ध होना अनिवार्य था।
4. जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने में रूस की अनिच्छा (Unwillingness of Russia to enter into war against Japan):
चाहे रूस जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को तैयार हो गया था पर वास्तव में उसने ऐसा अनिच्छापूर्वक किया था तथा वह इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। उसने इसके लिए कितनी ही शर्ते मित्र राष्ट्रों से मनवाईं, फिर भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तभी की जब अमेरिका ने जापान पर अणु बम्ब का प्रहार किया तथा उसकी हार निश्चित हो गई।
5. ईरान तथा टर्की में रूसी हस्तक्षेप (Russian intervention in Iran and Turkey):
द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा रूस की सेनाएं ईरान में प्रवेश कर गई थीं। ईरान के उत्तरी भाग पर रूस की सेनाओं का अधिकार था। पश्चिमी राष्ट्रों ने उसके इस कदम को सर्वथा अनुचित बताकर अपना क्षोभ प्रकट किया तथा रूस को चेतावनी भी दी। उन्होंने इन देशों की सुरक्षा सम्बन्धित कुछ कदम भी उठाए क्योंकि यह देश नहीं चाहते थे कि रूस अपनी विस्तारवादी नीति के अन्तर्गत इन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। इससे भी दोनों पक्षों में कटुता में वृद्धि हुई तथा शीत युद्ध को प्रोत्साहन मिला।
6. यूनान में रूस का हस्तक्षेप (Russian Intervention in Greece):
1944 में हुए एक समझौते के अन्तर्गत रूस ने यूनान पर इंग्लैण्ड का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। इंग्लैण्ड ने यूनान पर अधिकार करने के बाद वहां के साम्यवादी दल का विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप 1945 में होने वाले चुनावों में राज्यसत्तावादियों की विजय तथा साम्यवादियों की पराजय हुई। इस पर साम्यवादियों ने यूनान की सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटेन इस हाल में नहीं था, कि इस विद्रोह का मुकाबला कर पाता इसलिए उसने यूनान से अपनी सेनाएं वापस हटाने का निश्चय किया।
पश्चिमी देशों के अनुसार इस साम्यवादी विद्रोह में स्पष्ट रूप से रूस का हाथ था। उनके अनुसार यूनान के पड़ोसी साम्यवादी राज्य यूनान के विद्रोहियों की सहायता कर रहे थे। इस प्रकार पश्चिमी देशों के लिए रूस का बढ़ता प्रभाव चिन्ता का विषय था जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने ‘ट्रमैन सिद्धान्त’ (Trueman Doctrine) के अन्तर्गत यूनानी सरकार की आर्थिक सहायता का निश्चय किया और यही सिद्धान्त शीत युद्ध की दिशा में पश्चिम की ओर से एक महत्त्वपूर्ण कदम था, इस प्रकार यूनान में रूसी हस्तक्षेप ने भी शीत युद्ध के बढ़ाने में योगदान दिया।
7. जर्मनी पर भारी क्षति तथा अन्य समस्याएं (Heavy reparation on Germany and other roblems):
इसमें कोई सन्देह नहीं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक हानि रूस को उठानी पड़ी थी इसलिए उसने याल्टा सम्मेलन में जर्मनी से क्षतिपूर्ति के लिए 10 अरब डालर की मांग की, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने इस मांग को भविष्य में विचार करने के लिए मान लिया पर रूस ने इसको अन्तिम मान्यता समझा तथा उसने जर्मनी के उद्योग को नष्ट करते हुए सभी मशीनों का रूस में स्थानान्तरण करना आरम्भ कर दिया।
इससे पहले से ही अस्त-व्यस्त जर्मन अर्थव्यवस्था और भी अधिक छिन्न-भिन्न हो गई। इससे अमेरिका तथा इंग्लैण्ड काफ़ी नाराज़ हुए क्योंकि उनको ‘जर्मनी की आर्थिक सहायता करनी पड़ी यही नहीं रूस ने जर्मनी से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का भी उल्लंघन किया।
8. रूस द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार तथा अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियां (Anti-American propaganda by Russia and Communist activities in America): युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूसी समाचार-पत्रों प्रावदा (Pravada) तथा इजवेस्तिया (Izvestia) इत्यादि ने अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान आरम्भ कर दिया। इनमें आलोचनात्मक लेख इत्यादि प्रकाशित होने लगे जिनसे अमेरिका के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में भारी क्षोभ फैला।
9. संयुक्त राष्ट्र में रूस का व्यवहार (Russian behaviour in the U.N.):
संयुक्त राष्ट्र अभी अपना कार्य ठीक ढंग से चला भी न पाया था कि रूस ने अपने निषेधाधिकार (Veto Power) का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया।1961 तक अमेरिका ने इस अधिकार का प्रयोग एक बार भी नहीं किया जबकि रूस ने इस काल में 65 बार इसका प्रयोग किया था। इस पर पश्चिमी राष्ट्रों ने यह धारणा बना ली कि रूस ने अपने निषेधाधिकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को ठुकराने की नीति अपना ली है तथा वह संयुक्त राष्ट्र को असफल है। इससे भी दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। – शीतयुद्ध के लिए पश्चिमी गुट किस प्रकार ज़िम्मेदार था ? इसके लिए प्रश्न नं0 3 देखें।
प्रश्न 3.
शीतयुद्ध को बढ़ावा देने में पश्चिमी गुट किस प्रकार ज़िम्मेदार था ?
उत्तर:
शीतयुद्ध को बढ़ावा देने में कुछ हाथ पश्चिमी गुट का भी था। जिस प्रकार पश्चिमी राज्यों ने अपनी शिकायतों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शीतयुद्ध के कारणों के लिए रूस उत्तरदायी था उसी प्रकार रूस को पश्चिमी देशों से काफ़ी शिकायतें थीं। इसलिए रूस के अनुसार युद्ध के बाद के तनाव तथा कटुता के लिए उत्तरदायित्व पश्चिमी देशों का था। रूस की पश्चिमी देशों के विरुद्ध अग्रलिखित शिकायतें थीं
1. अमेरिका की विस्तारवादी नीति (Extentionist Policy of America):
साम्यवादी लेखकों के अनुसार शीत युद्ध का प्रमुख कारण अमेरिका की संसार पर प्रभुत्व जमाने की साम्राज्यवादी आकांक्षा में निहित है। वे कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने जर्मनी तथा इटली को धूल में मिलते हुए देखा है। चीन गृह युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैण्ड प्रथम श्रेणी की शक्ति से तृतीय श्रेणी की शक्ति बन चुका था। फ्रांस की विजय मात्र औपचारिक थी। इस प्रकार जो एक मात्र पूंजीवादी देश बिना खरोंच खाए विश्व शक्ति के रूप में उभरा था वह अमेरिका था।
युद्ध के अन्त में वह एकमात्र अणु शक्ति था। उसके नियन्त्रण में दुनिया की 60% दौलत थी। उसके पास शक्तिशाली जलसेना तथा शायद सबसे शक्तिशाली वायुसेना थी क्योंकि अमेरिका का आन्तरिक ढांचा पूंजीवादी था। अतः सरकारी मशीनरी बड़े-बड़े करोड़पतियों के हाथ में थी जिनका एकमात्र उद्देश्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना था। अमेरिका के विश्व प्रभुत्व के स्वप्न के रास्ते में एकमात्र रुकावट रूस द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध था तथा इसी कारण अमेरिका रूस से घृणा करता था।
2. युद्ध के समय रूस के सन्देह (Doubts of Russia during the War):
1945 में जर्मनी को पता चल गया था कि वह अधिक देर तक नहीं लड़ सकेगा। जर्मनी का यह विचार था कि यदि वह पश्चिमी राष्ट्रों से कोई समझौता कर लेता है तथा उनके सामने समर्पण करता है तो पश्चिमी देश उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। वे जो भी व्यवहार करेंगे वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होगा।
परन्तु यदि वे रूस के सामने समर्पण करते हैं तो रूस निश्चय ही उनके साथ बुरा व्यवहार करेगा क्योंकि उन्होंने रूस पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे तथा उनको डर था कि यदि वे रूस के सामने समर्पण करते हैं तो वह अवश्य ही उनसे बदला लेगा। अत: वे रूस के सामने समर्पण नहीं करना चाहते थे।
जर्मनी के साथ समर्पण की बातचीत चल रही थी। जर्मनी पूर्व में बहत ज़ोर से लड रहा था पर पश्चिम में उसने हथियार डालने आरम्भ कर दिए थे। रूस ने इस बात पर सन्देह किया कि कहीं पश्चिमी राष्ट्र नाजियों के साथ कोई समझौता न कर ले। रूज़वैल्ट की मृत्यु पर ट्रमैन अमेरिका का राष्ट्रपति बना जो और भी ज़्यादा रूस विरोधी था। इसलिए रूस को और भी अधिक सन्देह हुआ कि कहीं अमेरिका जर्मनी से कोई गुप्त सन्धि न कर ले।
रूस ने अमेरिका पर यह आरोप भी लगाया कि उसने इटली तथा फ्रांस के फासिस्ट तत्त्वों से सम्पर्क स्थापित किया था। उधर ब्रिटेन भी यूनान में साम्यवाद विरोधी लोगों का समर्थन कर रहा था। रूस को यह भी शिकायत थी कि फिनलैण्ड के साथ उसका युद्ध छिड़ने तथा उसके द्वारा लैनिनग्राड पर आक्रमण किए जाने पर भी अमेरिका ने काफी समय तक उससे अपने राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किए थे। इस प्रकार युद्ध के काल में पश्चिमी राष्ट्रों की कुछ ऐसी गतिविधियां रहीं जो रूस के सन्देह का स्पष्ट कारण थीं।
3. पश्चिम द्वारा रूस के सुरक्षा हितों की अवहेलना (Western Block ignored Russian interest about its defence):
ज्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो रूस तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को स्थापित करने की एक होड़ लग गई थी। रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों से ये कभी नहीं पूछा कि वे अपने अधिकृत प्रदेशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना करने जा रहे हैं। परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों ने इस बात पर बल दिया कि रूस अपने अधिकृत देशों में स्वतन्त्र निर्वाचनों के आधार पर प्रजातन्त्र की स्थापना करे।
परन्तु रूस ऐसा नहीं करना चाहता था। पश्चिमी राष्ट्र इन देशों में युद्ध से पहले वाली व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे पर ये पुरानी सरकारें रूस विरोधी थीं। अत: रूस अपने सुरक्षा हितों को देखते हुए इन देशों में किस प्रकार अपनी विरोधी सरकारों की स्थापना करवा सकता था जब कि पश्चिमी देश ऐसा करने पर बल दे रहे थे। अपने अधिकृत क्षेत्रों में सरकारें बनाते समय उन्होंने रूस की बात भी न पूछी थी। इस प्रकार रूस का नाराज़ होना स्वाभाविक था।
4. पश्चिमी देशों द्वारा युद्ध के समय द्वितीय मोर्चा खोलने में देरी (Delay in opening second front by Western Countries during the War):
जब फ्रांस की हार हो गई तथा जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो इंग्लैण्ड तथा अमेरिका ने अपने ही हितों को ध्यान में रखते हुए रूस की सहायता करने की सोची, रूस ने इन दोनों देशों को फ्रांस की ओर से बार-बार दूसरा मोर्चा खोलने को कहा ताकि युद्ध का जो सारा दबाव इस समय रूस पर पड़ा था जर्मनी के दो स्थानों पर लड़ने के कारण कम हो जाए, परन्तु इन दोनों देशों ने यह बहाना बनाकर कि अभी हम तैयारी नहीं हुई है दूसरा मोर्चा खोलने में पर्याप्त विलम्ब किया जिसका परिणाम यह निकला कि युद्ध का सारा बोझ अकेले रूस पर पड़ा जिसके परिणामस्वरूप रूस को धन-जन की भारी हानि उठानी पड़ी।
रूस को मालूम हो गया कि यदि वह स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे अपने तथा जर्मनी के बीच के राज्यों पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। उसका यह इरादा भांप कर चर्चिल ने जब दूसरा मोर्चा खोलने की बात की तो कहा कि हमारी सेनाएं फ्रांस की ओर से नहीं बलकान प्रायद्वीप से होकर उत्तर की ओर बढ़े। इस बात ने रूस के सन्देह की और भी पुष्टि कर दी।
5. युद्ध के समय पश्चिम द्वारा रूस की अपर्याप्त सहायता (Insufficient aid by West during War):
रूस को पश्चिमी देशों से यह भी शिकायत थी कि उन्होंने युद्ध काल में रूस की अत्यन्त अल्प मात्रा में सहायता की। 1941-42 के आरम्भिक काल में जो सहायता पश्चिमी राज्यों ने रूस को दी वह रूस द्वारा उत्पन्न कुल युद्ध सामग्री का केवल 4% थी। वास्तव में पश्चिमी राष्ट्र यह चाहते थे कि रूस जर्मनी के साथ लड़कर कमजोर हो जाए।
इसलिए उन्होंने उसकी बहुत कम सहायता की वह भी तब जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि जर्मनी द्वारा रूस को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाना स्वयं उनके अपने हित में नहीं था। 1943 में अवश्य उन्होंने इसलिए सहायता में वृद्धि की थी। पर तब तक रूस को यह विश्वास हो चुका था कि पश्चिमी राष्ट्र वास्तव में उसकी सहायता न करके उसे निर्बल बना देना चाहते हैं।
6. लैण्डलीज कानून को समाप्त करना (End of Land Lease):
युद्ध काल में रूस को अमेरिका से लैण्डलीज कानून के अन्तर्गत सहायता मिल रही थी। रूस पहले इसी सहायता से असन्तुष्ट था क्योंकि यह सहायता अपर्याप्त थी। फिर भी रूस समझता था कि युद्ध के बाद अपने पुनर्निर्माण के लिए भी उसको अमेरिका से सहायता मिलती रहेगी। पर ब I (Trueman) राष्ट्रपति बना जो रूस विरोधी था। उसने लैण्डलीज कानून को बन्द कर दिया तथा वह थोड़ी-सी सहायता भी बन्द कर दी। उधर पश्चिमी देश रूस के क्षतिपूर्ति के दावों का भी विरोध कर रहे थे। इससे रूस को विश्वास हो गया कि पश्चिमी देश उसकी समृद्धि तथा प्रगति को नहीं देखना चाहते।
7. एटम बम्ब का रहस्य गुप्त रखना (Secret of Atom Bomb):
अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति पर एटम बम्ब का आविष्कार कर लिया था। अमेरिका तथा रूस युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्र थे। रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया था पर अमेरिका ने एटम बम्ब के रहस्य को रूस से सर्वथा गुप्त रखा जबकि इंग्लैण्ड तथा कनाडा को इसका पता था।
इस बात से स्टालिन बड़ा क्षुब्ध हुआ तथा उसने इसको एक भारी विश्वासघात माना इसका परिणाम यह निकला कि न केवल दोनों की मित्रता टूट गई बल्कि रूस ने अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित होकर अस्त्र-शस्त्र बनाने में लग गया और उसने भी केवल “वर्षों में ही अणु बम्ब का आविष्कार कर लिया। इसके बाद तो दोनों में शस्त्रास्त्रों की एक होड़ लग गई जिसने शीत युद्ध को प्रोत्साहित करने में बहुत योगदान दिया।”
8. पश्चिम द्वारा रूस विरोधी प्रचार अभियान (Anti-Russian Propaganda by West):
युद्ध काल में ही पश्चिमी देशों की प्रैस रूस विरोधी प्रचार करने लगी थी। बाद में तो पश्चिमी राज्यों ने खुले आम रूस की आलोचना करनी आरम्भ कर दी। जिस रूस ने जर्मनी की पराजय को सरल बनाया उसके विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का यह प्रचार उसको क्षुब्ध करने के लिए पर्याप्त था। मार्च, 1946 में चर्चिल ने अपने फुल्टन भाषण में स्पष्ट कहा था
“हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे के संस्थापन को रोकना चाहिए।” यह दूसरा स्वरूप साम्यवाद के सिवाय और क्या हो सकता है ? राष्ट्रपति ट्रमैन ने उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन वाणिज्य सचिव को इस बात पर त्याग-पत्र देने के लिए कहा कि उन्होंने रूस तथा अमेरिका की मैत्री की बात कही न ने सीनेट के सामने रूस की नीति को स्पष्ट रूप से आक्रामक बताया था। इस प्रकार इस प्रचार ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें दोनों एक-दूसरे के प्रति घृणा, वैमनस्य की भावना में डूब गए।

प्रश्न 4.
द्वि-ध्रुवीयकरण के विकास के कारणों को लिखिए। (Write the causes of the development of Bi-polarisation.)
उत्तर:
द्वि-ध्रुवीय विश्व के विकास के निम्नलिखित कारण थे
1. शीत युद्ध का जन्म-द्वि-ध्रुवीय विश्व के विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारण शीत युद्ध था। शीत युद्ध के कारण ही विश्व अमेरिकन एवं सोवियत गुट के रूप में दो भागों में विभाजित हो गया था।
2. सैनिक गठबन्धन-द्वि-ध्रुवीय विश्व का एक कारण सैनिक गठबन्धन था। सैनिक गठबन्धन के कारण अमेरिका एवं सोवियत संघ में सदैव संघर्ष चलता रहता था।
3. पुरानी महाशक्ति का पतन-दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा जापान जैसी पुरानी महाशक्तियों का पतन हो गया तथा विश्व में अमेरिका एवं सोवियत संघ दो ही शक्तिशाली देश रह गए थे इस कारण विश्व द्वि-ध्रुवीय हो गया।
4. अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका-द्वि-ध्रुवीय विश्व का एक अन्य कारण अमेरिका का विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना भी था।
5. कमज़ोर राष्ट्रों को आर्थिक मदद-अमेरिका एवं सोवियत संघ विश्व के निर्धन एवं कमजोर राष्ट्रों को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देते थे, जिस कारण अधिकांश निर्धन एवं कमज़ोर राष्ट्र दोनों गुटों में से एक गुट के साथ ही लेते थे।
6. शस्त्रीकरण-द्वि-ध्रुवीय विश्व का एक अन्य कारण शस्त्रीकरण था। दोनों गुट एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए शस्त्रों की दौड़ में लगे रहते थे।
7. विकास की इच्छा-अमेरिका एवं सोवियत संघ की अधिक-से-अधिक विकास की इच्छा ने भी दोनों देशों को एक-दूसरे के विरुद्ध कर दिया, तथा विश्व द्वि-ध्रुवीय हो गया।
8. परस्पर प्रतियोगिता-अमेरिका एवं सोवियत संघ में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतियोगिता शुरू कर दी, इस कारण भी विश्व द्वि-ध्रुवीय विश्व की ओर मुड़ने लगा।
प्रश्न 5.
द्वि-ध्रुवीय विश्व की चुनौतियों का वर्णन करें। (Discuss the challenges of Bipolarity.)
उत्तर:
द्वि-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था शीत युद्ध के दौरान स्थापित हुई थी जब विश्व दो गुटों में बंट गया था, एक गुट .. का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान ही द्वि-ध्रुवीय . विश्व को चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती गुट-निरपेक्ष आन्दोलन (NAM) तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (New International Economic Order-NIEO) की थीं, जिनका वर्णन इसं प्रकार है
1. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन (Non-aligned Movement-NAM):
शीत युद्ध के दौरान द्वि-ध्रुवीय विश्व को सबसे बड़ी चुनौती गट-निरपेक्ष आन्दोलन से मिली। शीत युद्ध के दौरान जब विश्व तेज़ी से दो गटों में बंटता जा रहा था, तब गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने विश्व के देशों, विशेषकर विकासशील एवं नव स्वतन्त्रता प्राप्त देशों को एक तीसरा : विकल्प प्रदान किया, जिससे ये देश किसी गुट में शामिल होने की अपेक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी विदेशी नीति का: संचालन कर सकें। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में की गई।
गुट निरपेक्ष आन्दोलन को शुरू करने में भारत के प्रधानमन्त्री श्री पं० जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रॉन टीटो तथा मिस्त्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अब तक सम्मेलन हो चुके हैं। 1961 में इसके 25 सदस्य थे, जोकि अब बढ़कर 120 हो गए हैं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने दोनों गुटों में पाए जाने वाले शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया, इसने इसे एक अव्यावहारिक तथा खतरनाक नीति माना।
इसके साथ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की नीति सदैव नाटो, वारसा पैक्ट, सीटो तथा सैन्टो जैसे सैनिक गठबन्धनों से दूर रहने की रही है, जिनका निर्माण अमेरिकी एवं सोवियत गुटों ने किया था। वास्तव में ऐसे सैनिक गठबन्धन प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देकर विश्व शान्ति को खतरा उत्पन्न करते हैं। गुट-निरपेक्ष देश प्रत्येक विषय पर उसके गुण-दोष के अनुसार विचार करते हैं, न कि किसी महाशक्ति के आदेश के अनुसार । अतः स्पष्ट है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सदैव द्वि-ध्रुवीय विश्व के लिए चुनौती बना रहा है।
2. नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (New International Economic Order-NIEO):
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के साथ-साथ नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने भी सदैव द्वि-ध्रुवीय विश्व को चुनौती दी है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा तीसरे विश्व के देशों ने पुरानी विश्व अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के जन्म तथा स्थापना को प्रोत्साहित किया। 70 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मुख्य विषय बन गया।
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं सम्बन्धी समझौते करना, बचाववाद (Protectionism) को समाप्त करना तथा पुरानी परम्परावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करना है। 70 के दशक में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु विभिन्न संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, गट-निरपेक्ष आन्दोलन, विकसित देशों व विकासशील देशों ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए।
राष्ट्र संघ की महासभा के छठे विशेष अधिवेशन में महासभा ने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ-साथ गुट-निरपेक्ष देशों ने भी नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयास किया। विकासशील देशों को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के पश्चात् नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने एक ऐसा संघ उपलब्ध करवाया है जहां से ये विकासशील द्वि-ध्रुवीय विश्व के ताने-बाने से बच सकें।
प्रश्न 6.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रकृति का वर्णन करें।
उत्तर:
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय उपनिवेशवादी प्रणाली के विघटन के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कई ऐसे घटक उपस्थित हुए जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति और रंग-रूप को बदल दिया। इन घटकों में एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में नए राज्यों के उदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन उत्पन्न किया। “इन राष्ट्रों का यत्न अन्तर्राष्ट्रीय खेल को इस प्रकार परिवर्तित करना है जिससे अनेक राष्ट्रीय हितों की पर्ति हो और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो और उस ऐतिहासिक प्रक्रिया की समाप्ति हो जिसने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था।”
अधिकांश नए राज्यों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे आन्दोलन को चुना जिसे गुट-निरपेक्षता (Non alignment) की संज्ञा दी जाती है। Belgrade Conference (1961) से लेकर Harare Conference (1986) तक गुट-निरपेक्षता का समूचा इतिहास इन नए देशों के उपर्युक्त उद्देश्य को ही ध्वनित करता है। प्रो० के० पी० मिश्रा के शब्दों में “गुट-निरपेक्षता एक ऐसा सैद्धान्तिक योगदान है जो लोकप्रिय हो रहा है और जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मूल परिवर्तन लाए जाने के लिए उचित वातावरण उत्पन्न कर रहा है।”
गुट-निरपेक्षता का जन्म (Origin of Non-alignment)-वास्तव में गुट-निरपेक्षता का जन्म भारत में हुआ। सुबीमल दत्त ने अपनी पुस्तक ‘With Nehru in the Foreign Office’ में यह लिखा है-“राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हरिपुरा सत्र (1939) में गुट-निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया गया था।” हमा और दर्शन भी गुट-निरपेक्षता को स्वीकार करते हैं। गांधी जी के शब्दों में “भारत को सभी का मित्र होना चाहिए और किसी का भी शत्रु नहीं होना चाहिए।” स्वतन्त्रता से पूर्व भी जब जवाहर लाल नेहरू अन्तरिम सरकार में विदेशी मामलों का कार्यभारी था, उसने यह घोषणा की थी कि भारत गुटों से पृथक् रहेगा।
1946 में दोबारा उसने घोषणा की कि भारत अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति बनाएगा। उसके अपने शब्दों में-“यथासम्भव हम गुटों से दूर रहना चाहते हैं। इन गुटों के कारण ही युद्ध हुए हैं और इनके कारण पहले से भी अधिक भयंकर युद्ध हो सकते हैं।” बर्मा के प्रधानमन्त्री ने 1948 में यही बात कही थी “ब्रिटेन, अमेरिका और रूस इन तीनों बड़ी शक्तियों के साथ बर्मा के मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने चाहिएं।” 1950 में फिर यह घोषणा की गई कि बर्मा किसी एक गुट के विरुद्ध किसी दूसरे गुट के साथ सम्बद्ध नहीं होना चाहता।” स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इंडोनेशिया ने भी इस भावना को प्रकट किया।
कई विद्वान् गुट-निरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध में मानते हैं। गुट-निरपेक्ष देशों की 1973 की Algier’s Conference में इस बात की चर्चा की गई कि गुट-निरपेक्षता शीत युद्ध का परिणाम है अथवा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का परिणाम है। Fidel Castro ने यह तर्क दिया कि गुट-निरपेक्षता उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन है।
F. N. Haskar के शब्दों में-“जहां तक भारत का सम्बन्ध है गुट-निरपेक्षता का आरम्भ बेलग्रेड में नहीं हुआ। न ही इसका आरम्भ अप्रैल, 1955 में बाण्डंग में हुए अफ्रीकन-एशियन राष्ट्रों के सम्मेलन में हुआ। इसकी जड़ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध किए गए स्वतन्त्रता संग्राम में है और नेहरू और गांधी द्वारा प्रदर्शित विचारों और विश्व दृष्टिकोण में है।”
हम यह कह सकते हैं कि चाहे यह संगठनात्मक रूप शीतयुद्ध के दौरान मिला किन्तु निश्चित रूप से यह शीतयुद्ध की उपज नहीं है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ (Meaning of Non-alignment)-जैसे कि ऊपर कहा गया है कि गुट-निरपेक्षता की जड़ें द्वितीय महायुद्ध के बाद के उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संघर्षों में है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ है उस शीतयुद्ध में विचार, निर्णय तथा कार्य की स्वतन्त्रता बनाए रखना जो सैनिक तथा अन्य गठजोड़ों को प्रोत्साहन देता है।
इसका उद्देश्य शान्ति और सहयोग के क्षेत्रों को विस्तृत करना है। अतः गुट-निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश को प्रत्येक मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतन्त्रता; उसे राष्ट्रीय हित के आधार पर और विश्व शान्ति के आधार पर निर्णय लेने की स्वतन्त्रता न कि किसी निर्धारित दृष्टिकोण के आधार पर या किसी बड़ी शक्ति से गठजोड़ होने के आधार पर निर्णय लेना।
गुट-निरपेक्षता की प्रकृति (Nature of Non-alignment) अधिकांश पाश्चात्य विद्वान् इस शब्द में ‘Non’ लगे होने के कारण इसे नकारात्मक अवधारणा समझते हैं। वे इसे तटस्थता समझ लेते हैं क्योंकि यह शीतयुद्ध के प्रति प्रतिक्रिया है। वे इसे उभरते राष्ट्रवाद की एक आंशिक उपज समझते हैं। अफ्रीको-एशियन राष्ट्रवाद धुरी प्रणाली की एक क्रिया है। उसकी सही प्रकृति निम्नलिखित विचार बिन्दुओं में दर्शाई जा सकती है
1. गुट-निरपेक्षता तटस्थता नहीं है (Non-alignment is not Neutrality):
गुट-निरपेक्षता की अवधारणा तटस्थता की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। तटस्थता का अर्थ किसी भी मुद्दे पर उसके गुण-दोषों के भिन्न उसमें भाग न लेना है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ है, पहले से ही किसी मुद्दे पर उसके गुण-दोषों को दृष्टि में रखे बिना अपना दृष्टिकोण तथा पत्र बनाए रखना।
इसके विपरीत गुट-निरपेक्षता का अर्थ है अपना दृष्टिकोण पहले से ही घोषित न करना। कोई भी गुट-निरपेक्ष देश किसी भी मुद्दे के पैदा होने पर उसे अपने दृष्टिकोण से देखकर निर्णय करता था, न कि किसी बड़ी शक्ति के दृष्टिकोण से देखकर। तटस्थता की धारणा केवल युद्ध के समय संगत है और तटस्थता का अर्थ है अपने आपको युद्ध से अलग करना। परन्तु गुट-निरपेक्षता की धारणा युद्ध एवं शान्ति दोनों में प्रासंगिक है।
2. राष्ट्र हित और अन्तर्राष्ट्रवाद का समन्वय (Synthesis of National Interest and Internationalism):
विश्व में शान्ति बनाए रखने के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का अर्थ है राष्ट्र हित और अन्तर्राष्ट्रवाद का समन्वय। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं ने इस आन्दोलन को अपनी पुरातन सभ्यता की परम्पराओं पर तथा पाश्चात्य उदारवादी परम्पराओं पर आधारित किया है।
3. विश्व शान्ति की चिन्ता (Concern for World Peace):
गुट-निरपेक्षता आन्दोलन का सम्बन्ध विश्व में शान्ति स्थापना करना है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि आधुनिक युद्ध बहुत थोड़े समय में सारे विश्व को नष्ट कर सकता है। साथ ही गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हिंसात्मक ढंग से हल करने के विरुद्ध हैं। उनके विचार में युद्ध समस्या को सुलझाने के स्थान पर उसे और जटिल बना देता है।
4. आर्थिक सहायता लेना (Seeking Economic Assistance):
गुट-निरपेक्षता आन्दोलन में सम्मिलित होने वाले सभी देश अविकसित हैं अथवा विकासोन्मुखी हैं। गुट-निरपेक्ष देशों ने आर्थिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का यत्न किया है। उन्होंने अपने साधनों को इकट्ठा करके विकसित देशों पर अपनी निर्भरता को घटाने का यत्न किया है। गट-निरपेक्ष देशों में से भारत आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करके इन देशों के लिए उदाहरण बनने जा रहा है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय की स्वतन्त्रता (Independence of Judgement on International Issues):
गुट-निरपेक्षता आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सम्मिलित होने वाले देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर अपना निर्णय करने में स्वतन्त्र हैं।
6. उपनिवेशवाद तथा जातिवाद का विरोध (Opposition to Colonialism and Racialism):
गुट निरपेक्ष देश उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरोधी हैं। सुकार्नो तथा नेहरू विशेष तौर पर इस बात से सम्बन्धित थे कि उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष बल पकड़ जाएगा। गुट-निरपेक्ष देशों, विशेषतः भारत ने Zimbabve Rhodesia की स्वतन्त्रता के लिए विशेष समर्थन दिया था। दक्षिणी अफ्रीका में अपनाए जा रहे जातिवाद का भी गुट-निरपेक्षता आन्दोलन ने विरोध किया है।
7. शक्ति की राजनीति का विरोध (Opposition to Power Politics):
Morgenthau तथा Schwar zenberger अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को शक्ति के लिए संघर्ष मानते हैं। शक्ति का अर्थ किसी विशेष व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों पर नियन्त्रण। गुट-निरपेक्षता कम-से-कम सिद्धान्त में शक्ति की राजनीति का एक खेल है। यह प्रभाव राजनीति (Influence Politics) में विश्वास रखती है। प्रभाव राजनीति शक्ति की राजनीति से इस दृष्टि से भिन्न है कि यह समझाने-बुझाने (Persuasion) में विश्वास रखती है जबकि शक्ति बल द्वारा दूसरों से अपनी इच्छा का काम करवाना चाहती है।
8. नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना (Establishment of New International Economic Order) :
इस तथ्य के होते हुए भी कि नये राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, आर्थिक दृष्टि से अब भी विकसित देश उन पर हावी हैं। वे ऐसी आर्थिक प्रणाली में बंधे हुए हैं जो निर्धनों और अविकसित देशों का शोषण कर रखती हैं।

प्रश्न 7.
‘गुट-निरपेक्ष आन्दोलन’ से आप क्या समझते हैं ? इसके मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन करें।
अथवा
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष का अर्थ-इसके लिए प्रश्न नं० 6 देखें। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त-गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं
- सदस्य देशों संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता एवं सुरक्षा की रक्षा करना।
- साम्राज्यवाद, रंगभेद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन करना।
- विकासशील एवं विकसित देशों के बीच पाई जाने वाली असमानता को दूर करना।
- शस्त्रों की होड़ को रोककर निःशस्त्रीकरण को लागू करना।
- एक देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना।
- गट-निरपेक्ष देशों को आत्म-निर्भर बनाने का प्रयास करना।
प्रश्न 8.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में होने वाली गतिविधियों में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।
अथवा
‘तटस्थता’ व ‘गुट-निरपेक्षता’ में अन्तर स्पष्ट कीजिए। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका बताइए।
उत्तर:
तटस्थता तथा गुट-निरपेक्षता में अन्ग-तटस्थता युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति से सम्बन्धित है, जबकि गुट-निरपेक्षता युद्ध और शान्ति दोनों से सम्बनि तटस्थता एक नकारात्मक धारणा है, जो किसी पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने से रोकती है, जबकि गुट निरपेक्ष एक सकारात्मक नीति है जो विषय के महत्त्व के अनुसार उसमें किसी गुट-निरपेक्ष राष्ट्र की रुचि निर्धारित करती है।
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट-निरपेक्षता की नीति को लागू करने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू को है। गुट-निरपेक्षता को विचार से नीति एवं नीति से आन्दोलन बनाने में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत ने सदैव गुट-निरपेक्ष का सम्मान एवं समर्थन किया। भारत की भूमिका निर्गुट आन्दोलन की हर गतिविधि में अहम रही है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में होने वाली गतिविधियों में भारत ने निम्नलिखित भूमिका अभिनीत की है
(1) भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का जन्मदाता है।
(2) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विश्व शान्ति पर बल देता है। भारत के प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्वितीय शिखर सम्मेलन में विश्व शान्ति के लिए पांच सूत्री प्रस्ताव पेश किया जिसमें मुख्यतः-सीमा विवादों को विवेक एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने, अणु शस्त्रों के निर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने एवं संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करने पर बल दिया।
(3) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सातवां शिखर सम्मेलन 1983 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ।
(4) 1983 में भारत के प्रयत्नों से बहुत-सी समस्याओं-ईरान-इराक युद्ध, कम्पूचिया की समस्या, हिन्द महासागर में शान्ति बनाए रखना एवं पारस्परिक आर्थिक सहयोग आदि पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।
(5) नाम (NAM) के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर सर्वसम्मति प्राप्त करके एवं गुट-निरपेक्ष तथा विश्व के देशों के हितों की रक्षा करके इस आन्दोलन को ओर भी शक्ति प्रदान की।
(6) नाम के अध्यक्ष के रूप में भारत ने पूर्ण निशस्त्रीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया।
(7) 1985 में घोषित नई दिल्ली घोषणा पत्र श्री राजीव गांधी के निशस्त्रीकरण सम्बन्धी चार सूत्रीय योजना पर आधारित था।
(8) राजीव गांधी की अध्यक्षता में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग, उत्तर-दक्षिण, उत्तर-दक्षिण वार्तालाप, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका आदि विषयों पर जोर दिया।
(9) भारत की पहल पर ‘अफ्रीका कोष’ कायम किया गया।
(10) भारत ने अफ्रीका कोष को, 50 करोड़ रु० की राशि दी।
(11) भारत को 1986 एवं 1989 में अफ्रीका कोष का अध्यक्ष चुना गया। ऋण, पूंजी-निवेश तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे कई आर्थिक प्रस्तावों का मूल प्रारूप भारत ने बनाया।
(12) 1989 के बेलग्रेड सम्मेलन में भारत ने पृथ्वी संरक्षण कोष कायम करने का सुझाव दिया और सदस्य राष्ट्रों ने इसका भारी समर्थन किया।
(13) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दसवें शिखर सम्मेलन में भारत ने विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण, वातावरण सुरक्षा, आतंकवाद जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। भारत का यह रुख जकार्ता घोषणा में शामिल किया गया कि आतंकवाद प्रादेशिक अखण्डता एवं राष्ट्रों की सुरक्षा को एक भयानक चुनौती है।
(14) भारत ने ही गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का ध्यान विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण की तरफ खींचा।
(15) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के महत्त्व एवं सदस्य राष्ट्रों की इसमें निष्ठा बनाए रखने के लिए भारत ने द्विपक्षीय मामले सम्मेलन में न खींचने की बात कही जिसे सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया।
(16) 1997 में दिल्ली में गट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का शिखर सम्मेलन हआ।
(17) बारहवें शिखर सम्मेलन में भारत ने विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण, विश्व शान्ति एवं आतंकवाद से निपटने के लिए एक विश्वव्यापी सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका सदस्य राष्ट्रों ने समर्थन किया।
(18) तेरहवें शिखर सम्मेलन में सक्रिय भूमिका अभिनीत करते हुए भारत ने आतंकवाद एवं इसके समर्थकों की कड़ी आलोचना कर विश्व शान्ति पर बल दिया।
(19) भारत ने क्यूबा में हुए 14वें, मिस्र में हुए 15वें तथा इरान में हुए 16वें शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया।
(20) भारत ने वेनुजुएला में हुए 17वें एवं अजरबैजान में हुए 18वें शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए विकास के लिए वैश्विक शांति की स्थापना पर बल दिया।
अत: गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका सदैव सराहनीय रही है।
प्रश्न 9.
शीत-युद्धोपरान्त काल में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की व्याख्या करो।
उत्तर:
शीत युद्ध के पश्चात् आज की बदली हुई परिस्थितियों में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका में भी बदलाव आया है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन नए विश्व के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है जो शान्ति, मैत्री एवं सम्पन्नता से परिपूर्ण हो। वातावरण समय में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका एवं महत्त्व दोनों ही बढ़ा रहा है या ऐसा कहा जाए कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन की बढ़ती भूमिका ने उसे महत्त्वपूर्ण आन्दोलन बना दिया है।
विश्वीकरण की तीव्र होती प्रक्रिया के कारण विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों ने खुला बाजार नीति को अपनाया है। विकसित देशों की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां विकासशील देशों में पूंजी निवेश करती हैं ताकि दोनों राष्ट्रों को लाभ हो। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ऐसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता है। आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन शक्ति गुटों में नहीं अपितु विकसित एवं विकासशील देशों में आर्थिक सम्बन्धों में सन्तुलन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।
आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सदस्य राष्ट्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहा है। अब यह विकसित देशों से विकासशील एवं पिछड़े देशों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी मदद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के लिए समर्पित है। कार्टाजेना सम्मेलन में परमाणु हथियारों के समूल नाश के लिए धीमे एवं सीमित प्रयासों पर सदस्य राष्ट्रों ने चिंता व्यक्त की।
बारहवें शिखर सम्मेलन में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने एवं उन्हें नष्ट करने के लिए एक बहु-पक्षीय समझौते पर बल दिया। इस सम्मेलन में निशस्त्रीकरण एवं आतंकवाद से निपटने के लिए विश्वव्यापी सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया गया।
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अमीर एवं विकसित राष्ट्रों के प्रभुत्व से निकालने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तत्पर है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन यह देखता है कि कोई एक शक्ति केन्द्र सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व न कायम कर ले। विश्व को महायुद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन इसके सदस्य राष्ट्र अहम् भूमिका निभा रहे हैं।
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विश्वव्यापी दरिद्रता को दूर करने की कोशिश कर रहा है। कोलंबिया सम्मेलन में विकासशील देशों में भूख, ग़रीबी, निरक्षरता तथा पेयजल की कमी से निपटने के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया। लन अब संयक्त राष्ट्र संघ में सधार के लिए भी मांग करता है यह इसे अमेरिका की दादागिरी से बचाने के लिए प्रयासरत है। अतः गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका शीत युद्ध के बाद बढ़ गई है।
अब यह केवल नव स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही नहीं प्रयासरत अपितु अपने विश्वव्यापी स्वरूप के कारण अब यह विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण, विश्वशान्ति एवं सुरक्षा, सम्पन्नता, आर्थिक-सामाजिक उन्नति, सहयोग एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रयासरत है। अब गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विश्वव्यापी समस्याओं एवं मामलों की ओर भी ध्यान दे रहा है।
प्रश्न 10.
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ?
अथवा
नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का पतन होना आरम्भ हो गया था। साम्राज्यवादी व औपनिवेशिक शक्तियों की पकड़ अपने उपनिवेशों पर ढीली पड़ने लगी थी क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बैल्जियम आदि इस स्थिति में नहीं थे कि वे अपने उपनिवेशों पर अपना कब्जा जमा सकें। अतः उन्होंने अपने अपने उपनिवेशों को आजाद करना आरम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 50 व 60 के दशक में एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के सैंकड़ों देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर उभरे।
सदियों तक यूरोपीय देशों ने इन क्षेत्रों पर अपना नियन्त्रण बनाए रखा और इन देशों का शोषण किया। इन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण कर करके यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मज़बूत बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का लगा। इसलिए इस युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक पुनरुत्थान और एकीकरण की तरफ ध्यान देना आरम्भ कर दिया ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें।
नव-स्वतन्त्र अथवा विकासशील देशों को अपनी आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए विकसित देशों की मदद की आवश्यकता थी। राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा नए देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने के कारण संयुक्त राष्ट्र की संख्या तिगुनी हो गई थी। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा तीसरे विश्व के देशों ने पुरानी विश्व अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (New International Economic Order) के जन्म तथा स्थापना को प्रोत्साहित किया। 70 के दशक में इन विकासशील देशों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता की मांग भी आरम्भ कर दी जिसके परिणामस्वरूप एक नई अवधारणा नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ। यह 70 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मुख्य विषय बन गया।
नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है ? (What is NIEO ?)-नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य-सामग्री उपलब्ध कराना है, साधनों को विकसित देशों में विकासशील देशों में भेजना, वस्तओं सम्बन्धी समझौते करना, बचाववाद को समाप्त करना तथा पुरानी परम्परावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना है। 70 के दशक में इन विकासशील देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की क्योंकि अमेरिका व यूरोपीय देश इस बात के लिए सदैव तत्पर रहे कि विकासशील देशों की तैयार वस्तुएं अमेरिका व यूरोपीय आर्थिक बाजार में प्रवेश न कर सकें।
पुरानी व्यवस्था विकासशील अथवा कम विकसित अथवा तृतीय विश्व के हितों की अवहेलना करते हुए बनाई गई है जिसका उद्देश्य विकसित राष्ट्रों के हितों व उनकी आवश्यकताओं की रक्षा करना है जबकि विकासशील देशों का उद्देश्य यह है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तहत विकसित राष्ट्रों के लिए एक आचार संहिता बनाकर तथा कम विकसित राष्ट्रों के उचित अधिकारों को मानकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सबके लिए समान तथा न्यायपूर्ण बनाना है।’
“नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विश्वास विकासशील देशों में सहयोग स्थापित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाना है। इसका विश्वास विश्व में एक ऐसी लोकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित करना है जिससे प्रत्येक राष्ट्र को समानता का व्यवहार मिले और ऐसी आर्थिक स्थिति बने जिससे विश्व में उसका राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हो सके।” 70 के दशक के बाद इन विकासशील देशों ने आर्थिक समानता की मांग करनी आरम्भ कर दी। विकासशील राष्ट्र बिना किसी देरी के उत्तर-दक्षिणी वार्ता की मांग करते हैं। परन्तु विकसित राष्ट्र किसी भी कीमत पर इस तर्क को स्वीकार नहीं करते जिसके कारण इनके मध्य विवाद (Conflict) पैदा हो गया।
इस विवाद को उत्तर-दक्षिणी विवाद (North-South Conflict) के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वे भू-मध्य रेखा के उत्तर में और विकासशील देश भू-मध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। उस समय की आर्थिक व्यवस्था संकटों के दौर में से गुजर रही थी। इस समय तक विकसित देशों में भी एक स्थायित्व की स्थिति आ चुकी थी अर्थात् विकसित देशों ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक विकास थम गया था। मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही थी। मुद्रा स्फीति की समस्या पर रोक लगाने हेतु ही विकासशील देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग जोरों से आरम्भ कर दी।
यह विश्व के आर्थिक साधनों के आदर्श विभाजन पर बल देती है तथा ऐसे साधनों को उपाय में लाना चाहती है जिससे कि ग़रीब देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। इस व्यवस्था को जन्म देने में मुख्यतः तीन बातें सामने आती हैं-प्रथम, विकसित देशों को विकासशील देशों के साथ अपनी पूंजी में भाग देना चाहिए।
द्वितीय, मुद्रा स्फीति की बढ़ती हुई दर पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि इस नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाए। ततीय, आर्थिक साधनों के आदर्श विभाजन के लिए विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों पर दबाव डालना। वास्तव में, इस अवधारणा ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया के घनिष्ठ सम्बन्ध को उभार कर सामने रखा है। जब तक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती तब तक न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी स्थापित नहीं की जा सकती।
पुरानी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं (Features of the Old Economic Order): विकसित देशों द्वारा स्थापित पुरानी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं
(1) पुरानी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विश्व में पूर्वी व पश्चिमी गुटों में अन्तर पाया जाता था, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के मुद्दे को लेकर उत्तर-दक्षिण में भी विवाद था।
(2) पुरानी आर्थिक व्यवस्था विकसित देशों के हितों की रक्षा करती थी जिससे सारा लेन-देन विकसित देशों में ही होता था जो कि भेदभाव रहित उदारवादी व्यापार पर आधारित था जिससे विश्व में खुले व्यापार की नीति को प्रोत्साहन मिला।
(3) पुरानी अर्थव्यवस्था राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत थी। इस पर कुछेक राष्ट्रों का एकाधिकार था। यह व्यवस्था तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और असंगत थी।
(4) पुरानी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकसित राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को इस तरह नियमित कर रखा था कि विकसित देशों को विकासशील देशों में आसान शर्तों पर माल बेचने की छूट प्राप्त थी।
80 के दशक के अन्त तक विकसित देशों को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कई साम्यवादी देशों का पतन हो गया और वहां प्रजातान्त्रिक सरकारों की स्थापना हुई। इस दशक में विकासशील देशों ने भी उत्तर-दक्षिण विवाद की बजाए उत्तर-दक्षिण वार्ता (North-South Dialogue) पर बल देना आरम्भ कर दिया। 1975 तक इन विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय धन-सम्पदा आदि का पूरा उपभोग विकसित राष्ट्रों ने किया। विकसित देशों का मत था कि अगर विकासशील देश पिछड़ गए हैं तो उनके पीछे उनकी पिछड़ी तकनीक है, जिसके कारण वे अपनी प्राकृतिक सम्पदा का उपभोग नहीं कर पाए हैं।
इसीलिए विकासशील देशों ने पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को खत्म करना चाहा। पुरानी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तीन भाग थे प्रथम-पश्चिमी देशों की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था द्वितीय-उत्तर-दक्षिण की निर्भरता की व्यवस्था तृतीया- पूर्व-पश्चिम की स्वतन्त्रता की व्यवस्था पूर्वी देश अपनी आत्मनिर्भरता के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। इस व्यवस्था में विकासशील देशों की कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं थी।
विश्व अर्थव्यवस्था पर कुछेक विकसित देशों का एकाधिकार है। विश्व का मुनाफा भी इन्हीं देशों के हाथ में है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण धन तथा व्यापारिक मण्डियों पर एकाधिकार था। जिसका कच्चे माल की मण्डियों पर नियन्त्रण होगा उसका तैयार माल की मण्डियों पर नियन्त्रण होना स्वाभाविक है। इस तरह इन विकसित देशों ने अविकसित तथा विकासशील देशों का दोहरा शोषण किया जिससे विकसित व विकासशील देशों में असमानता फैल गई।
उपर्युक्त आधारों पर ही 70 के दशक में विकासशील देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की ताकि ये देश अपना आर्थिक विकास कर सकें। विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश अपने देशों के अतिरिक्त साधनों को विकासशील देशों को दे दें ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विकासशील देश लाभ उठा सकें। यदि इस दिशा में विकासशील राष्ट्र प्रगति करते हैं तो इससे विकसित देशों को भी फायदा होगा और नई मण्डियां प्राप्त होंगी। चूंकि अब इन देशों ने लम्बी परतन्त्रता के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है।
अतः विकसित देशों का नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि वे इन देशों की आर्थिक मदद करें ताकि ये देश भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो सके। नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत प्रयत्नों द्वारा विकसित देश विकासशील देशों को अपनी आय का 0.7% भाग ही देने को तैयार हुए हैं जोकि बहुत कम हैं।
नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धान्त (Basic Principles of NIEO) विकासशील देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ बुनियादी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है
- कच्चे माल की कीमत को घटाने-बढ़ाने पर रोक लगाई जाए तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अन्तर न होना।
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों पर समुचित प्रतिबन्ध,
- विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना,
- विश्व मौद्रिक व्यवस्था का सामान्यीकरण करना,
- खनिज पदार्थों और सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर किसी राष्ट्र की सम्प्रभुता की स्थापना करना।
- विकासशील देशों द्वारा तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- दोनों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को समाप्त करना।

प्रश्न 11.
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा किये गए प्रयासों का वर्णन करें।
उत्तर:
70 के दशक में नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हेतु विभिन्न संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, विकसित देशों व विकासशील देशों ने विभिन्न स्तरों पर यत्न किए। इन संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन इस प्रकार है
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयत्न (UN efforts at the establishment of NIEO)
(क) 1 मई, 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के छठे विशेष अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना में उठाए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों को निश्चित किया जैसे कि
- व्यापार व विकास सम्बन्धी प्रारम्भिक कच्चे माल की समस्याओं को हल किया जाए।
- अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था और विकासशील देशों की वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी मामलों को निपटाया जा सके।
- विकासशील देशों द्वारा अत्यधिक औद्योगिकीकरण की दिशा में प्रयास हो।
- विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को तकनीक का हस्तान्तरण किया जाए।
- बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों व निगमों की गतिविधियों का संचालन तथा नियन्त्रण।
- राज्यों के आर्थिक कार्यों व कर्तव्यों का एक चार्टर बनाया जाए जिसमें प्रत्येक राज्यों के अधिकार व कर्त्तव्य का वितरण हो।
- विकासशील देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग पर बल।
(ख) व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) सितम्बर, 1975 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग’ पर सातवां विशेष अधिवेशन उत्तर-दक्षिण वार्ता के लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें तृतीय विश्व तथा पश्चिमी दोनों द्वारा अपनी समझौता वार्ताओं पर यथार्थवाद का प्रदर्शन किया गया। 77 का समूह (Group of 77) तथा पश्चिम के बीच सहानुभूतिपूर्व सहयोग के फलस्वरूप समझौता पास हुआ जो तीसरे विश्व की प्रगति के मार्ग में मील का पत्थर प्रमाणित हुआ।
इन सभी सम्मेलनों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सम्प्रभु, समानता तथा सहयोग के आधार पर स्थापित करने हेतु पुनर्गठित करना है ताकि इनमें से भेदभाव को हटाकर इसे न्याय पर आधारित किया जा सके। अंकटाड के कई सम्मेलनों ने इस दिशा में कार्य किए जैसे-प्रगतिशील सिद्धान्तों का निर्माण, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को विकसित किया जाए, पक्षपातपूर्व रवैये की समाप्ति, सांझी निधि का निर्माण किया जाए जिससे विकासशील देशों के ऋण का भार कम हो सके।
(ग) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के प्रयास-नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन ने भी अपने स्तर पर प्रयास आरम्भ कर दिए। इस संगठन (UNIDO) का उद्देश्य तीसरे विश्व के देशों का औद्योगिक विकास करना है। इस दिशा में इसने कुछ महत्त्वपूर्ण सम्मेलन बुलाए।
2. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा किए गए प्रयास (Efforts of NAM) एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका ने नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों ने मिलकर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आरम्भ किया था। यह नव-स्वतन्त्र राष्ट्र अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के रूप में एकत्र हुए। साम्राज्यवादी आर्थिक ढांचे से दबे हुए इन देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्मित करने का प्रयत्न किया। गुट-निरपेक्ष देशों के लुसाका सम्मेलन (1970) में इन देशों की आर्थिक समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया गया। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों के 1975 के
लीमा सम्मेलन (LIMA Conference) में आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक संहति कोष (So Fund) की स्थापना की स्वीकृति दी गई। 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के सातवें शिखर सम्मेलन में भारत की पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिलाया। इसके अतिरिक्त G-15 के विभिन्न सम्मेलनों में भी इसकी स्थापना की दिशा में मांग उठाई गई।
3. विकसित देशों के प्रयास (Efforts of Developed Countries):
80 के दशक के आरम्भ में पूर्व व बाद में विकसित देशों को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि तेल उत्पादक देशों ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अतः विकसित देशों ने भी नई व्यवस्था की ओर ध्यान देना शरू किया। विकासशील देशों की मांगों की तरफ विकसित देशों ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना आरम्भ कर दिया था।
विकसित देशों को आर्थिक विकास व सहयोग के संगठन (OECO) विश्व बैंक, IMF तथा GATT आदि ने बचाववाद (Protectionism) की नीति को छोड़कर उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। विकासशील देशों ने भी उत्तर-दक्षिण विवाद की जगह उत्तर-दक्षिण वार्ता पर बल देना आरम्भ कर दिया। काफ़ी प्रयत्नों के द्वारा विकसित देश विकासशील देशों को अपनी आय का 0.7% हिस्सा देने को तैयार हो गए।
4. विकासशील देशों के प्रयास (Efforts of Developing Countries):
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल सभी देश विकासशील देश हैं, परन्तु विकासशील देशों में सभी गुट-निरपेक्ष देश शामिल नहीं हैं। विकासशील देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की दिशा में निम्नलिखित प्रयत्न किए
(1) संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 1974 में हुए सम्मेलन में विकासशील देशों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की।
(2) विकासशील देशों ने अंकडाट में विभिन्न सम्मेलनों में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को मनवाने के लिए प्रयत्न किए।
(3) विकासशील देशों ने 1977 के पेरिस में सम्पन्न Conference on Trade Co-operation में भी मांग उठाई। इस सम्मेलन में उत्तर-दक्षिण के देशों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किए।
(4) 1982 में विकासशील देशों का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ। इसमें विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनाने और पारस्परिक सहयोग के आठ बिन्दुओं पर भारत की पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बल दिया।
इस प्रकार विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र व उसके बाहर के सम्मेलनों, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलनों, राष्ट्र मण्डल के शिखर सम्मेलनों, G-15 एवं G-77 के सम्मेलनों में इस मांग को उठाकर लोकमत बनाने की कोशिश की। जी 15 की नौवीं बैठक जमैका (Jamaica) में फरवरी, 1999 में हुई और इसमें 17 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विश्व आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों को अधिक भागीदारी दिए जाने की मांग की गई। यह भी सुझाव दिया गया कि WTO, WB तथा IMF जैसी आर्थिक संस्थाओं में अधिक सहयोग व तालमेल होना चाहिए।
प्रश्न 12.
शीत युद्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही ? गुट-निरपेक्षता की नीति ने किस प्रकार भारत का हित साधन किया ?
उत्तर:
शीत युद्ध के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट-निरपेक्ष नेता के रूप में उभर कर भारत ने न केवल स्वयं को अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों से अपने आपको अलग रखा, बल्कि नव स्वतन्त्रता प्राप्त देशों एवं विकासशील देशों को भी दोनों शक्ति गुटों से अलग रखने का प्रयास किया।
स्वतन्त्रता के पश्चात् पं० जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा तथा अन्य कई स्थानों पर यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा और भारत गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगा। पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह भी स्पष्ट किया था कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति उदासीनता नहीं है।
सन् 1949 में प्रधानमन्त्री नेहरू ने अमरीकी कांग्रेस के समक्ष भाषण देते हुए कहा था, “जहां स्वतन्त्रता खतरे में हो न्याय खतरे में हो या यदि कहीं आक्रमण किया जा रहा हो वहां हम उदासीन नहीं रह सकते और न ही रहेंगे। हमारी नीति उदासीनता की नीति नहीं है। हमारी नीति यह है कि शान्ति स्थापना के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्न किया जाए तथा जहां तक सम्भव हो सके शान्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जाए।”
उदाहरण के लिए 50 के दशक में हुए कोरिया युद्ध एवं स्वेज नहर के संकट को समाप्त करने के लिए भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने शीत युद्ध के दौरान उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जो दोनों शक्ति गुटों में से किसी के साथ नहीं जुड़े थे।
यद्यपि कई आलोचकों का यह कहना है कि गुट-निरपेक्षता का आदर्श भारत के राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों से मेल नहीं खाता, परन्तु यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि भारत न केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतन्त्र निर्णय ले सका, बल्कि ऐसे पक्ष का साथ देता था, जिससे भारत को लाभ हो। इसके साथ-साथ दोनों महाशक्तियों ने भारत से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास किया, यदि एक गुट भारत के विरुद्ध होता तो दूसरा गुट भारत की मदद को आ जाता था।
यद्यपि कई आलोचक भारत की गुट-निरपेक्षता को सिद्धान्तहीन एवं विरोधाभासी बताते हैं। क्योंकि भारत ने सन् 1971 में सोवियत संघ से एक बीस वर्षीय सन्धि कर ली थी। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन परिस्थितियों में इस प्रकार की सन्धि करना भारत के लिए आवश्यक हो गया था। अधिकांश तौर पर भारत ने दोनों गुटों से अलग रहने की नीति ही अपनाई।
भारत ने निम्नलिखित ढंग से अपना हित साधन किया
1. आर्थिक पुनर्निर्माण- भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाकर अपना आर्थिक पुनर्निर्माण किया क्योंकि किसी गुट में शामिल न होने से उसे सभी देशों से सहायता प्राप्त होती रही।
2. स्वतन्त्र नीति निर्माण- भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाकर स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी नीतियों का निर्माण किया।
3. भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी-गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई।
4. दोनों गुटों से अधिक सहायता-गुट-निरपेक्ष देश होने के कारण भारत को दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती रही।
प्रश्न 13.
भारतीय गुट-निरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारतीय गुट-निरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है
1. भारत की निर्गुटता की नीति उदासीनता की नीति नहीं है-भारत की निर्गुटता की नीति उदासीनता की नीति नहीं है क्योंकि भारत ने स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय राज्य नीति से दूर नहीं रखा है, अपितु भारत अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका अभिनीत करता है।
2. सैन्य समझौतों का विरोध-भारत सैन्य समझौतों का विरोध करता है। अतः भारत सेन्टो (CENTO), नाटो (NATO), सीटो (SEATO), वारसा सन्धि (WARSA-PACT) आदि में सम्मिलित नहीं हुआ है।
3. शक्ति राजनीति से दूर रहना-भारत शक्ति राजनीति का विरोध करता है और प्रत्येक राष्ट्र के शक्तिशाली बनने के अधिकार को स्वीकार करता है।
4. शान्तिमय सह-अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की नीति-भारत का पंचशील के सिद्धान्तों पर पूर्ण विश्वास है। शान्तिमय सह-अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की नीति पंचशील के दो प्रमुख सिद्धान्त हैं। भारत शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का समर्थन करता है।
5. स्वतन्त्र विदेश नीति-भारत अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति पर कार्यान्वयन करता है। भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण किसी भी अन्य देश के प्रभावाधीन नहीं करता, अपितु स्वेच्छा से स्वतन्त्र रूप में करता है। भारत दोनों शक्ति गुटों में से किसी भी गुट का सदस्य नहीं है।
6. निर्गुट देशों के मध्य गुटबन्दी नहीं है-कुछ आलोचकों का मत है कि निर्गुटता की नीति गुट-निरपेक्ष देशों की गुटबन्दी है। किन्तु आलोचकों का यह विचार उचित नहीं है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ गुट-निरपेक्ष देशों का तृतीय गुट स्थापित करना नहीं है।
प्रश्न 14.
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म कैसे हुआ ? UNCTAD ने 1972 की अपनी रिपोर्ट में किन सुधारों को प्रस्तावित किया ?
उत्तर:
नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म- इसके लिए प्रश्न नं० 10 देखें। UNCTAD द्वारा दिये गए सुधार-UNCTAD ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रस्ताव दिये
- अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण प्राप्त होगा, जिनका दोहन एवं दुरुपयोग विकसित कर सकते हैं।
- अल्पविकसित देश विकसित देशों के बाज़ार में भी अपना माल बेच सकेंगे।
- विकसित देशों से आयातित प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी।
- अल्पविकसित देशों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी।
प्रश्न 15.
भारत द्वारा गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाने के मुख्य कारण लिखिए।
उत्तर:
भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति को जोश में आकर नहीं अपनाया बल्कि यह गम्भीर चिन्तन का फल था और इसको अपनाने के मुख्य कारण इस प्रकार थे थिक पुननिर्माण-प्रथम, भारत कई वर्षों के साम्राज्यवादी शोषण के बाद स्वतन्त्र हुआ था और इसके सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का था। यह कार्य शान्ति के वातावरण में हो सकता था न कि तनावपूर्ण स्थिति में। अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य न बनना ही उचित था क्योंकि यदि भारत किसी गुट में सम्मिलित होता तो इससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती जोकि भारत के लिए ठीक नहीं थी।
2. स्वतन्त्र नीति निर्धारण के लिए-द्वितीय, भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति इसलिए भी अपनाई क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयता प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र रहने की उत्कट अभिलाषी थी। भारत को स्वतन्त्रता हजारों देश-प्रेमियों के बलिदान के बाद मिली थी। अतः भारतीयों के लिए स्वतन्त्रता अमूल्य थी। किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ इस मूल्यवान् स्वतन्त्रता को खो बैठना था। भारत यह अनुभव करता था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे भाग लेने का पूर्ण अधिकार है और यदि भारत किसी गुट में शामिल हो जाता तो भारत को अपना यह अधिकार खो देना पड़ता। अत: पूर्ण स्वतन्त्रता की इच्छा के कारण भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया।
3. भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए-तृतीय, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ठीक गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया।
4. शान्ति का समर्थक-गुट-निरपेक्षता की नीति का ऐतिहासिक आधार पर भी समर्थन किया जाता है। भारत का इतिहास यह बताता है कि भारत ने सदैव शान्ति की नीति का अनुसरण किया है। उसकी कभी भी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षाएं नहीं रहीं। इस प्रकार गुट-निरपेक्षता की नीति भारत के परम्परागत दर्शन तथा आदर्शों की आधुनिक युग में राजनीतिक अभिव्यक्ति है।
5. दोनों गुटों से आर्थिक सहायता- भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की जा सके और हुआ भी ऐसा ही। भारत दोनों गुटों द्वारा मिलने वाली सहायता का आनन्द उठाता रहा। यदि भारत एक ही गुट में शामिल हो जाता तो शायद वह न केवल एक ही गुट की सहायता लेता बल्कि दूसरे गुट वाले देश भारत को घृणा की दृष्टि से देखते।
6. भौगोलिक दशा-भारत की भौगोलिक दशा ऐसी थी कि यदि भारत पश्चिमी या साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो उसके अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो जाता।
7. एशिया के हित के लिए-एशिया के नए स्वतन्त्र राष्ट्रों में पश्चिम के प्रति घृणा थी और भारत को सभी एशियाई देश प्रतिष्ठा से देख रहे थे। यदि भारत पश्चिमी गुट से मिल जाता तो एशिया के देशों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता। अन्य देश भी भारत के अनुसरण करते हुए पश्चिम में मिलना प्रारम्भ कर देते।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा दो गुटों के बीच व्याप्त उन बन्धों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। इसके अन्तर्गत दोनों गुट एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबन्धन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, अधिकाधिक शस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा लेते थे।
फ्लोरेंस एलेट तथा मिखाइल समरस्किल ने अपनी पुस्तक ‘A Dictionary of Politics’ में शीत युद्ध को “राज्यों में तनाव की वह स्थिति जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने तथा दूसरे को निर्बल बनाने की वास्तविक युद्ध के अतिरिक्त नीतियां अपनाता है” बताया है। – डॉ० एम० एस० राजन (Dr. M.S. Rajan) के अनुसार, “शीत युद्ध शक्ति-संघर्ष की राजनीतिक का मिला-जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिन्तन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक-दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है।”
पं० जवाहर लाल नेहरू (Pt. Jawahar Lal Nehru) के अनुसार, “शीत युद्ध पुरातन शक्ति-सन्तुलन की अवधारणा का नया रूप है, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है।”
प्रश्न 2.
शीत युद्ध के कोई चार परिणाम लिखिए।
उत्तर:
शीत युद्ध के परिणामों का वर्णन इस प्रकार है
1. विश्व का दो गुटों में विभाजन-शीत युद्ध का प्रथम परिणाम यह हुआ कि विश्व का दो गुटों में विभाजन हो अमेरिका के साथ हो गया, तो दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ हो गया।
2. सैनिक गठबन्धनों की राजनीति-शीत युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि इसके कारण सैनिक गठबन्धनों की उत्पत्ति हुई तथा सैनिक गठबन्धनों को शीत युद्ध के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अमेरिका ने जहां नाटो, सीटो तथा सैन्टो जैसे सैनिक गठबंधन बनाये, वहां सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया।
3. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति-शीत युद्ध के कारण गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति हुई। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य नव-स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्रों को दोनों गुटों से अलग रखना था।
4. शस्त्रीकरण को बढ़ावा-शीत युद्ध का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव यह पड़ा कि इससे शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। दोनों गुट एक-दूसरे पर अधिक-से-अधिक प्रभाव जमाने के लिए खतरनाक शस्त्रों का संग्रह करने लगे थे।

प्रश्न 3.
शीत युद्ध को बढ़ावा देने में सोवियत संघ किस प्रकार ज़िम्मेदार था ? कोई दो कारण बताएं।
उत्तर:
शीत युद्ध को बढ़ावा देने में सोवियत संघ निम्नलिखित कारणों से ज़िम्मेदार था
1. विचारधारा सम्बन्धित कारण (Ideological Reason):
पश्चिमी विचारधारा के अनुसार साम्यवाद के सिद्धान्त तथा व्यवहार में इसके जन्म से ही शीत युद्ध के कीटाणु भरे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर रूस द्वितीय विजेता के रूप में प्रकट हुआ था तथा यह द्वितीय महान् शक्ति था। अमेरिका तथा रूस वास्तव में दो ऐसी नधित्व करते हैं जिनमें कभी तालमेल नहीं हो सकता तथा जो पर्णतया एक-दसरे की विरोधी पद्धतियां हैं।
2. रूस की विस्तारवादी नीति (Extentionist Policy of Russia):
शीत युद्ध के लिए एक अन्य कारण के लिए भी पश्चिमी राज्य रूस को उत्तरदायी ठहराते हैं। उनका कहना है कि युद्ध के बाद भी रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखा। इस प्रकार अमेरिका के मन में उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में सन्देह होता चला गया, जिसको रोकने के लिए उसने भी कुछ कदम उठाए जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया।
प्रश्न 4.
शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका किस प्रकार ज़िम्मेदार था ?
उत्तर:
शीत यद्ध को बढावा देने में अमेरिका निम्नलिखित कारणों से जिम्मेदार था
1. अमेरिका की विस्तारवादी नीति (Extentionist Policy of America):
साम्यवादी लेखकों के अनुसार शीत युद्ध का प्रमुख कारण अमेरिका की संसार पर प्रभुत्व जमाने की साम्राज्यवादी आकांक्षा में निहित है।
2. एटम बम्ब का रहस्य गुप्त रखना (Secret of Atom Bomb):
अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति पर एटम बम्ब का आविष्कार कर लिया था।
3. पश्चिमी द्वारा रूस विरोधी प्रचार अभियान (Anti-Russian Propaganda by West):
युद्ध काल में ही पश्चिमी देशों की प्रैस रूस विरोधी प्रचार करने लगी थीं। बाद में तो पश्चिमी राज्यों ने खुले आम रूस की आलोचना करनी आरम्भ कर दी। जिस रूस ने जर्मनी की पराजय को सरल बनाया उसके विरुद्ध मित्र राष्ट्रों को यह प्रचार उसको क्षुब्ध करने के लिए पर्याप्त था।
4. अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाने का कार्यक्रम (American Programme of Occupation of Japan):
पहले यह निर्णय किया था कि कोरिया तथा मन्चूरिया में जापानी सेनाओं का आत्मसमर्पण रूस स्वीकार करेगा। पर तब यह पता नहीं था कि जापान इतना शीघ्र आत्म-समर्पण कर देगा। इसके लिए बाद में रूस की सहायता की आवश्यकता न पड़ी।
अणु बम्ब के आविष्कार तथा प्रयोग ने जापान को शीघ्र आत्म-समर्पण करने पर बाध्य कर दिया। अमेरिका ने जापान के लिए एक कमीशन बनाने का सुझाव दिया। इस बात से रूस को शक हो गया कि अमेरिका जापान पर अपना अधिकार जमाये रखना चाहता है। इस कारणों से दोनों में तनाव पैदा हो गया।
प्रश्न 5.
शीत युद्ध के कोई चार लक्षण लिखिए।
उत्तर:
(1) शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति भी है जिसे मूलतः ‘गर्म शान्ति’ कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शान्ति रहती है और न ही ‘वास्तविक युद्ध’ होता है, बल्कि शान्ति एवं युद्ध के मध्य की अस्थिर स्थिति बनी रहती है।
(2) शीत युद्ध, युद्ध का त्याग नहीं, अपितु केवल दो महाशक्तियों के प्रत्यक्ष टकराव की अनुपस्थिति माना जाएगा।
(3) यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है, किन्तु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है। जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता है।
(4) शीत युद्ध एक वाक्युद्ध था जिसके अन्तर्गत दो पक्ष एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे जिसके कारण छोटे-बड़े सभी राष्ट्र आशंकित रहते हैं।
प्रश्न 6.
नये शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर प्रभाव लिखें।
उत्तर:
नए शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पुराने शीत युद्ध के समय यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियां भूतपूर्व उपनिवेशों में अपना कार्य कर रही थीं पर अब उनका स्थान अमेरिका ने ले लिया है। वह इन देशों के प्रतिक्रियावादी शासनों का पक्ष लेता है। उसकी इस बात ने इन देशों के मार्क्सवादी नेताओं रूस की तरफ अधिक-से-अधिक झुकने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस प्रकार इन देशों के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण विकासशील राज्यों में मार्क्सवाद के फैलने का कारण बना। दूसरे नए शीत युद्ध में असंलग्न आन्दोलन को एक नई गति प्रदान की है तथा अधिक-से-अधिक राज्यों की इसमें सम्मिलित होने की सम्भावना है। यद्यपि तीसरे विश्व के कुछ राज्यों ने दोनों महाशक्तियों को उनकी सेनाएं या शस्त्र अपनी भूमि पर रखने की सुविधाएं दी हैं पर फिर वे अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के इच्छुक हैं।
इस प्रकार अधिक-से-अधिक राज्यों में असंलग्न आन्दोलन में शामिल होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसी प्रकार नए शीत युद्ध के कारण जिसके अन्तर्गत उच्चकोटि की शस्त्र तकनीक होड़ सम्बन्धित है। दोनों महाशक्तियों प्रत्यक्ष झगड़े की अपेक्षा विकासशील राज्यों में अप्रत्यक्ष टकराव में लगी रही हैं।
प्रश्न 7.
देतान्त से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में देतान्त शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता है। यह शब्द वास्तव में फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिथिलता। देतान्त के आज के अर्थ में सहयोग तथा प्रतियोगिता दोनों ही बातें आती हैं। इसका अर्थ अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों राज्यों में तनाव शैथिल्य से है अर्थात् दोनों राज्यों में जो पहले शीत युद्ध में लगे हुए थे तनाव में शिथिलता आई तथा वे प्रतियोगी रहते हुए भी एक-दूसरे से सहयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार यह दोनों के सम्बन्धों के सामान्यीकरण की विधि है। आपस में हानिकारक तनावयुक्त सम्बन्धों के स्थान पर मित्रतापूर्ण सहयोग की स्थापना से है। इस प्रकार 1970 के आस-पास अमेरिकन राष्ट्रपति निकसन तथा रूस के प्रधानमन्त्री खुश्चेव के प्रयत्नों से रूस तथा अमेरिका के आपसी तनाव में जो कमी आई तथा सम्बन्धों में जो कुछ समन्वय या सहयोग की भावना उत्पन्न हुई उसी के लिए शब्द देतान्त का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न 8.
देतान्त के उदय के क्या कारण थे ?
उत्तर:
देतान्त के उदय के निम्नलिखित कारण थे
(1) रूस तथा अमेरिका के बीच शस्त्रों की होड़ बढ़ती जा रही थी जिनसे नए-नए अधिक-से-अधिक घातक अणु शस्त्रों का निर्माण हो रहा था। संघर्ष की नीति पर चलने का परिणाम केवल आण्विक युद्ध के रूप में निकल सकता था। इसलिए उनको एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच तनाव तथा संघर्ष की अपेक्षा सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार अणु युद्ध के भय ने दोनों को निकट आने पर बाध्य कर दिया।
(2) अणु युद्ध की सम्भावना को कई अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने जैसे कोरिया का युद्ध तथा विशेषकर क्यूबा के संकट ने सिद्ध कर दिया था। अत: इन घटनाओं का भी दोनों राज्यों पर प्रभाव पड़ा तथा उन्हें आपसी तनाव को कम करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा।
(3) इसी प्रकार देतान्त के लिए उत्तरदायी एक कारण चीन तथा रूस के बीच बढ़ने वाले मतभेद थे। प्रारम्भ में तो रूस तथा चीन मित्र थे तथा इसमें रूस की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी पर 1962 के रूस तथा चीन में विवाद हो गया। अब रूस के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह चीन के सामने अपनी स्थिति को सुदृढ रखने के लिए अमेरिका से अपने सम्बन्धों को सुधारे।
(4) कुछ विचारकों का यह भी मत है कि रूस ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी अमेरिका से मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया।
प्रश्न 9.
पुराने शीत युद्ध और नये शीत युद्ध में अन्तर बताएं।
उत्तर:
पुराने शीत युद्ध और नये शीत युद्ध में निम्नलिखित अन्तर पाए जाते हैं
1. क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर अन्तर-पुराने शीत और नये शीत युद्ध में प्रथम अन्तर यह है कि पुराने शीत युद्ध की अपेक्षा नये शीत युद्ध का क्षेत्र अधिक व्यापक है।
2. हथियारों के आधार पर अन्तर-पुराने शीत युद्ध की अपेक्षा नये शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के पास अधिक परिष्कृत एवं घातक हथियार थे, इसमें परमाणु, जैविक व रासायनिक हथियार शामिल हैं।
3. स्वरूप के आधार पर अन्तर-पुराने शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिकन गुट द्वारा साम्यवाद का विरोध किया गया, वहीं नये शीत युद्ध के दौरान अमेरिकन गुट द्वारा केवल सोवियत संघ का विरोध किया गया।
4. सोवियत संघ एवं अमेरिका की मजबूरी-पुराने शीत युद्ध एवं नये शीत युद्ध में एक अन्तर यह है कि जहां पुराने शीत युद्ध को जारी रखना सोवियत संघ की मजबूरी थी, वहीं नया शीत युद्ध अमेरिकन गुट की मजबूरी था।
प्रश्न 10.
गुट-निरपेक्षता का क्या अर्थ है ? इसके मुख्य उद्देश्य बताइए।
उत्तर:
गुट-निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी शक्ति गुट में शामिल न होना और शक्ति गुटों के सैनिक बन्धनों व अन्य बन्धनों व अन्य सन्धियों से दूर रहना। पण्डित नेहरू ने कहा था, “जहां तक सम्भव होगा हम उन शक्ति-गुटों से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं।” गुट-निरपेक्षता का यह भी अर्थ है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतन्त्रता से करेगा न कि किसी गुट के दबाव में आकर।
गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति शीतयुद्ध का दौर उदासीनता नहीं है। स्वर्गीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी के अनुसार, “गुट-निरपेक्षता में न तो तटस्थता और न ही समस्याओं के प्रति उदासीनता है। इसमें सिद्धान्तों के आधार पर सक्रिय और स्वतन्त्र रूप में निर्णय करने की भावना निहित है।” भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति एक सकारात्मक नीति है, केवल नकारात्मक नहीं है।
गुट-निरपेक्षता के उद्देश्य-इसके लिए प्रश्न नं० 33 देखें।
प्रश्न 11.
क्या ‘गुट-निरपेक्षता’ का अभिप्राय तटस्थता है ? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
गुट-निरपेक्षता का अर्थ है किसी शक्तिशाली राष्ट्र का पिछलग्गू न बनकर अपना स्वतन्त्र मार्ग अपनाना। गुटों से अलग रहने की नीति का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ‘तटस्थता’ कदापि नहीं है। कई पाश्चात्य लेखकों ने गुट निरपेक्षता के लिए तटस्थता अथवा तटस्थतावाद शब्द का प्रयोग किया है उनमें मॉर्गेन्थो, पीस्टर लायन, हेमिल्टन, फिश आर्मस्ट्रांग तथा कर्नल लेवि आदि ने इस नीति के लिए तटस्थता शब्द का प्रयोग कर भ्रम पैदा कर दिया है। वास्तव में दोनों नीतियां शान्ति व युद्ध के समय संघर्ष में नहीं उलझतीं, परन्तु तटस्थता निष्क्रियता व उदासीनता की नीति है, जबकि गुट-निरपेक्षता सक्रियता की नीति है।
तटस्थ देश अन्तर्राष्ट्रीय विषयों या घटनाओं के सम्बन्ध में पूर्णतया निष्पक्ष रहते हैं और वे किसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना या विषय के सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करते हैं। गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के प्रति निष्पक्ष या उदासीन नहीं होते, अपितु वे इन विषयों में पूर्ण रुचि लेते हैं और प्रत्येक विषय के गुणों को सम्मुख रखते हुए उसके सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु स्वतन्त्र होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी अभिनीत करते हैं। अतः गुट-निरपेक्षता की नीति का अभिप्राय निष्पक्षता या उदासीनता की नीति नहीं है।
प्रश्न 12.
भारत की गुट-निरपेक्षता नीति की पांच प्रमुख विशेषताएं बताइए।
उत्तर:
- भारत किसी गुट का सदस्य नहीं है। भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति स्वतन्त्र है।
- भारत की गुट-निरपेक्ष विदेश नीति सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है।
- भारत की गुट-निरपेक्ष विदेश नीति साम्राज्यवाद के विरुद्ध है।
- भारत की गुट-निरपेक्ष नीति रंग भेदभाव की नीति के विरुद्ध है।
- भारत की गुट-निरपेक्ष नीति विकासशील देशों के आपसी सहयोग पर बल देती है।

प्रश्न 13.
शीतयुद्ध में भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के कोई चार कारण बताओ।
अथवा
शीत युद्ध के समय भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के कोई चार कारण लिखिए।
उत्तर:
भारत के गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कारण हैं
1. आर्थिक पुनर्निर्माण-स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण था। अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य न बनना ही उचित था ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके।
2. स्वतन्त्र नीति-निर्धारण के लिए-भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि भारत स्वतन्त्र नीति का निर्धारण कर सके। भारत को स्वतन्त्रता हजारों देश प्रेमियों के बलिदान के बाद मिली थी। किसी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ इस मूल्यवान् स्वतन्त्रता को खो बैठना था।
3. भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट-निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया। यदि भारत स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय देता तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी होगी और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
4. दोनों गुटों से आर्थिक सहायता- भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए भी किया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त की जा सके और हुआ भी ऐसा ही।
प्रश्न 14.
बांडुंग सम्मेलन (1955) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
अप्रैल, 1955 में बांडंग स्थान में एशिया और अफ्रीकी राष्टों का एक सम्मेलन हआ जिसमें 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार करने के साथ साथ इनका विस्तार भी किया, अर्थात् पांच सिद्धान्तों के स्थान पर दस सिद्धान्तों की स्थापना की गई। इस सम्मेलन में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया तथा महान् शक्तियों का अनावश्यक अनुसरण न करने पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में सभी राज्यों की पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने, किसी राज्य पर सैनिक आक्रमण न करने तथा किसी राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर बल दिया गया।
प्रश्न 15.
बेलग्रेड शिखर सम्मेलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 एशियाई तथा अफ्रीकी व एक यूरोपीय राष्ट्र ने भाग लिया। लैटिन अमेरिका में तीन राष्ट्रों ने पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में महाशक्तियों से अपील की गई कि वे विश्व शान्ति तथा निःशस्त्रीकरण के लिए कार्य करें तथा परमाणु परीक्षण न करें।
विश्व के सभी भागों तथा रूपों में उप-निवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद की घोर निन्दा की गई। सम्मेलन में अंगोला, कांगो, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया के स्वतन्त्रता संघर्षों का समर्थन किया गया। बेलग्रेड सम्मेलन में 20 सूत्रीय घोषणा-पत्र को स्वीकार किया गया। इस घोषणा-पत्र में कहा गया कि विकासशील राष्ट्र बिना किसी भय व बाँधा के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को प्रेरित करें। बेलग्रेड सम्मेलन गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में बहुत महत्त्व रखता है।
प्रश्न 16.
नेहरू और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब पूंजीवाद तथा साम्यवाद में वैचारिक विभाजन, नस्लवाद, पिछड़े देशों की स्वतन्त्र नीति निर्माण की इच्छा इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण के प्रमुख विषय थे। भारत की भी यह प्रबल इच्छा थी कि वह गुटीय राजनीति से दूर रहकर अपनी इच्छा से विदेश नीति का निर्माण करे। ऐसे में भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व एवं विचारधारा ने प्रमुख भूमिका निभाई। पं० नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को गुट-निरपेक्षता की नीति पर आधारित किया।
लेकिन यह गुट-निरपेक्षता नकारात्मक तथा तटस्थवादी नहीं थी बल्कि सकारात्मक थी। पं. नेहरू के शासनकाल में गुट-निरपेक्षता की नीति को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पं० नेहरू ने गुट-निरपेक्षता की नीति के आधार पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई।
एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतन्त्र देश गुट-निरपेक्षता की नीति के कारण ही पं० नेहरू और भारत सरकर को मानवता का प्रवक्ता मानते थे। नेहरू के कट्टर आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते थे कि उनकी नीति भारत की अन्तर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है। नेहरू के जीवित रहते गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कई ऊंचाइयों को छूने लगा था। हम आज भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की बुनियाद और उसका अस्तित्व नेहरू के ही परिपक्व नेतृत्व की देन है।
प्रश्न 17.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के किन्हीं दो संस्थापकों के नामों का उल्लेख कीजिए। पहला गुट-निरपेक्ष आन्दोलन शिखर सम्मेलन किन तीन कारकों की परिणति था ?
उत्तर:
गट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो मुख्य संस्थापकों में, भारत के प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू एवं युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज़ टीटो शामिल हैं। पहला गुट-निरपेक्ष आन्दोलन शिखर सम्मेलन निम्नलिखित तीन कारकों की परिणति था
(1) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के पाँचों संस्थापक देशों (भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया तथा घाना) के बीच सहयोग की इच्छा।
(2) प्रथम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की दूसरी परिणति शीत युद्ध का प्रसार और इसका बढ़ता हुआ दायरा था।
(3) 1960 के दशक में बहुत-से नव स्वतन्त्रता प्राप्त देशों का उदय हुआ, जिन्हें एक मंच की आवश्यकता थी और वो मंच गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने प्रदान किया।
प्रश्न 18.
क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट पर एक नोट लिखें।
उत्तर:
क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा-सा द्वीपीय देश है। क्यूबा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश है। 1960 के दशक में जब शीत युद्ध पूरे जोरों पर था, तब सोवियत संघ को इस बात की आशंका थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने साथ मिला लेगा। यद्यपि सोवियत संघ क्यूबा को हर तरह की सहायता देता था, परन्तु फिर भी इससे वह सन्तुष्ट नहीं था। अन्ततः 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करके वहां पर परमाणु प्रक्षेपास्त्र स्थापित कर दिये। इन प्रक्षेपास्त्रों के कारण अमेरिका पहली बार किसी देश के परमाणु हमले के निशाने पर आ गया।
इससे अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिकन राष्ट्रपति कनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को सोवियत लडाक बेडों को रोकने का आदेश दिया। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की सम्भावना पैदा हो गई। इसे ही क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कहा जाता है। युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध न करने का निर्णय किया तथा सोवियत संघ ने भी अपने जहाजों की गति या तो धीमी कर ली या वापस हो लिए।
प्रश्न 19.
शीत युद्ध के समय कोई भयंकर एवं विनाशकारी युद्ध नहीं हुआ, कोई चार कारण बताएं।
उत्तर:
- परमाणु युद्ध से होने वाली हानि को सहने में दोनों पक्ष सक्षम नहीं थे।
- दोनों पक्ष एक-दूसरे की शक्ति एवं पराक्रम से डरे हुए तथा आशंकित थे।
- युद्ध होने की स्थिति में इतना अधिक विनाश होता कि उसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता था।
- परमाणु युद्ध की स्थिति में इतना अधिक विनाश होता कि विजेता का निर्णय करना मुश्किल हो जाता।
प्रश्न 20.
शीत युद्ध की कोई चार सैनिक विशेषताओं का उल्लेख करें।
उत्तर:
- शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे।
- दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे।
- दोनों गुटों ने सैनिक गठबन्धन किये हुए थे।
- शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगियों से यह आशा की जाती थी कि वे तर्क पूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे।
प्रश्न 21.
नाटो संगठन के किन्हीं चार उद्देश्यों का वर्णन करें।
उत्तर:
- नाटो संगठन के सदस्य देश शान्ति के समय एक-दूसरे को आर्थिक सहयोग देंगे।
- एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा तथा सभी देश उसका मिलकर मुकाबला करेंगे।
- नाटो के सदस्य देशों के परस्पर आपसी विवाद को बातचीत द्वारा हल किया जाएगा।
- प्रत्येक देश अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करेगा।
प्रश्न 22.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से भारत को प्राप्त होने वाले कोई चार लाभ बताएं ।
उत्तर:
- गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने के कारण भारत वैश्विक मामलों में स्वतन्त्र भूमिका निभा सका है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से भारत को विभिन्न देशों से आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिली है।
- गुट-निरपेक्ष नीति अपनाने के कारण भारत दोनों गुटों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल रहा है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के कारण भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।
प्रश्न 23.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की कोई चार सीमाएं लिखें।
उत्तर:
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन देश राजनीतिक तथा आर्थिक विकसित देशों को कोई कठोर चुनौती नहीं दे पाए हैं।
- गुट निरपेक्ष आन्दोलन को भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों ने नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है।
- गुट निरपेक्ष आन्दोलन ईरान-इराक युद्ध को नहीं रोक पाया।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन इराक द्वारा कुवैत पर किये गए आक्रमण को नहीं रोक पाया।
प्रश्न 24.
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक प्रणाली के सुधार के लिए दिए किन्हीं चार प्रस्तावों का वर्णन करें।
उत्तर:
- विकासशील देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण होगा।
- विकासशील देश भी अप:’ माल पश्चिमी देशों में बेच सकते हैं।
- विकासशील देशों को कम लागत पर पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी।
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाया जाएगा।
प्रश्न 25.
उपनिवेशवाद के अर्थ की व्याख्या करें।
उत्तर:
उपनिवेशवाद का अर्थ है कि एक शक्तिशाली देश द्वारा कमज़ोर देश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर उनका आर्थिक शोषण करना। जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत के विरुद्ध करता था। जे० ए० हाब्सन के अनुसार, “उपनिवेशवाद, राष्ट्रीयता का प्राकृतिक बहाव है, इस परीक्षण, प्रतिनिधि संस्कृति को नए प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण में, जिनमें वे अपने आप को पाते हैं, प्रतिरोपित करने की औपनिवेशिक शक्ति से किया जा सकता है।”
प्रश्न 26.
शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को छोटे सहयोगियों की आवश्यकता क्यों थी ? कोई चार तर्क दें।
अथवा
महाशक्तियों को शीत युद्ध के युग में मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता क्यों थी ?
उत्तर:
- महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबन्धन इसलिए करती थीं, ताकि उन देशों से वे अपने हथियार एवं सेना का संचालन कर सकें।
- महाशक्तियां छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे।
- छोटे देश सैन्य गठबन्धन के अन्तर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था।
- महाशक्तियां छोटे देशों पर आसानी से अपनी इच्छा थोप सकती थीं।
प्रश्न 27.
गुट-निरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश को”अल्प विकसित देशों” का दर्जा क्यों दिया गया ?
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश को अल्प विकसित देश इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय, उपनिवेशवादी प्रणाली के विघटन के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कई ऐसे घटक उपस्थित हुए, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति और रंग-रूप को बदल दिया। इन घटकों में एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में नए राज्यों के उदय ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। परन्तु अधिकांश देश आर्थिक रूप से जर्जर स्थिति में थे। इसलिए इन्हें अल्प विकसित देश कहा जाता है।
प्रश्न 28.
ऐसी किन्हीं चार वास्तविकताओं का उल्लेख कीजिए जिसने विश्व राजनीति में शीत युद्ध के पश्चात् बदलाव लाया।
उत्तर:
शीत युद्ध के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से विश्व राजनीति में बदलाव आए–
- शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही दोनों गुटों में चलने वाला वैचारिक संघर्ष भी समाप्त हो गया और यह विवाद भी समाप्त हो गया कि क्या समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को परास्त कर सकेगी।
- शीत युद्ध के पश्चात् विश्व में शक्ति सम्बन्ध बदल गए तथा विचारों एवं संस्थाओं के सापेक्षिक प्रभाव भी बदल गए।
- शीत युद्ध के पश्चात् उदारीकरण एवं निजीकरण ने विश्व राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है।
- शीत युद्ध के पश्चात् उदारवादी लोकतान्त्रिक राज्यों का उदय हुआ, जो राजनीतिक जीवन के लिए सर्वोत्तम प्रणाली है।
प्रश्न 29.
गुट-निरपेक्षता का अर्थ न तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से अलग-अलग रहना था और न ही तटस्थता था। व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
गुट-निरपेक्षता की धारणा स्वयं को न तो अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से अलग ही रखती है और न ही वह तटस्थ रहती है अर्थात् गुट-निरपेक्षता. की धारणा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटना में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाती है। गुट-निरपेक्षता की अवधारणा तटस्थता की अवधारणा से बिलकुल भिन्न है।
तटस्थता का अर्थ किसी भी मुद्दे पर उसके गुण-दोषों के भिन्न उसमें भाग न लेना है। तटस्थता का अर्थ है, पहले से ही किसी मुद्दे पर उसके गुण-दोषों को दृष्टि में रखे बिना अपना दृष्टिकोण तथा पक्ष बनाए रखना। इसके विपरीत गुट-निरपेक्षता का अर्थ शीतयुद्ध का दौर है अपना दृष्टिकोण पहले से ही घोषित न करना।
कोई भी गुट-निरपेक्ष देश किसी भी मुद्दे के पैदा होने पर उसे अपने दृष्टिकोण से देखकर निर्णय करता था, न कि किसी बड़ी शक्ति के दृष्टिकोण से देखकर। तटस्थता की धारणा केवल युद्ध के समय संगत है और तटस्थता का अर्थ है अपने आपको युद्ध से अलग करना। परन्तु गुट-निरपेक्षता की धारणा युद्ध एवं शान्ति दोनों में प्रासंगिक है।
प्रश्न 30.
शीत युद्ध के चार कारण लिखें।
अथवा
शीत युद्ध के कोई चार प्रमुख कारण लिखिये।।
उत्तर:
1. विचारधारा सम्बन्धित कारण-पश्चिमी विचारधारा के अनुसार साम्यवाद के सिद्धान्त तथा व्यवहार में इसके जन्म से ही शीत युद्ध के कीटाणु भरे हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर रूस द्वितीय विजेता के रूप में प्रकट हुआ था तथा यह द्वितीय महान् शक्ति था। अमेरिका तथा रूस वास्तव में दो ऐसी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कभी तालमेल नहीं हो सकता तथा जो पूर्णतया एक-दूसरे की विरोधी पद्धतियां हैं।
2. रूस की विस्तारवादी नीति-शीत युद्ध के लिए एक अन्य कारण के लिए भी पश्चिमी राज्य रूस को उत्तरदायी ठहराते हैं। उनका कहना है कि युद्ध के बाद भी रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रखा। इस प्रकार अमेरिका के मन में उसकी विस्तारवादी नीति के बारे में सन्देह होता चला गया, जिसको रोकने के लिए उसने भी कुछ कदम उठाए जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया।
3. अमेरिका की विस्तारवादी नीति-साम्यवादी लेखकों के अनुसार शीत युद्ध का प्रमुख कारण अमेरिका की संसार पर प्रभुत्व जमाने की साम्राज्यवादी आकांक्षा में निहित था।
4. एटम बम का रहस्य गुप्त रखना-अमेरिका द्वारा सोवियत संघ से एटम बम का रहस्य गुप्त रखना भी शीत युद्ध का एक कारण है।
प्रश्न 31.
विकासशील देशों की मुख्य मांगें क्या हैं ? कोई चार बताएं।
अथवा
विकासशील देशों की किन्हीं चार मुख्य मांगों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
- विकासशील देशों की प्रथम मांग नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को लागू करना है, ताकि विकसित एवं विकासशील देशों में समानता आ सके।
- विकासशील देश सदैव इस बात की मांग करते रहे हैं कि विकसित देश उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए धन प्रदान करें, क्योंकि विकसित देशों ने विकासशील देशों का शोषण करके ही धन कमाया है।
- विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने लिए और अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका की मांग कर रहे हैं।
- विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना।
प्रश्न 32.
कठोर द्वि-ध्रुवीयता से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर:
कठोर द्वि-ध्रुवीयता से अभिप्राय शीत युद्ध के 1945 से 1955 के समय काल से लिया जाता है जब दोनों गुटों ने अपने-अपने सदस्य राज्यों को पूर्ण रूप से नियन्त्रित कर रखा था। इस समय काल में दोनों गुटों में शामिल कोई भी सदस्य राज्य अपनी आन्तरिक एवं विदेश नीति बनाने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं था, बल्कि उसे अपने गुट के नेता के अनुसार ही नीतियां बनानी पड़ती थीं। इसीलिए सदस्य राज्यों की नीतियां पूर्ण रूप से वाशिंगटन एवं मास्को के आस-पास ही घूमती थीं।
प्रश्न 33.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के किन्हीं चार उद्देश्यों का वर्णन करो।
उत्तर:
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को शक्ति गुटों से अलग रखना है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का उद्देश्य विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना है।
- सदस्य देशों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को समाप्त करना इसका एक मुख्य उद्देश्य रखा गया है।
प्रश्न 34.
क्या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट-निरपेक्ष आन्दोलन प्रासंगिक रह गया है ? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् गुट-निरपेक्ष आन्दोलन निम्नलिखित कारणों से प्रासंगिक है
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- यह आन्दोलन नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक है।
- विकसित एवं विकासशील देशों में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रासंगिक है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट करें।
अथवा
“शीत युद्ध” से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका तथा रूस अथवा दो गुटों के बीच व्याप्त उन कटु सम्बन्धों के इतिहास से है, जो तनाव, भय तथा ईर्ष्या पर आधारित है। इसके अन्तर्गत दोनों गुट एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबन्धन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप तथा अधिकाधिक शस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा लेते हैं।

प्रश्न 2.
शीत युद्ध की कोई दो परिभाषाएं दें।
उत्तर:
1. पं० नेहरू के अनुसार, “शीत युद्ध पुरातन सन्तुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर, दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है।”
2. जान फास्टरं डलेस के अनुसार, “शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था अच्छाई का बुराई के विरुद्ध, सही का ग़लत के विरुद्ध एवं धर्म का नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था।”
प्रश्न 3.
शीत युद्ध के कोई दो कारण बताएं।
उत्तर:
- पश्चिमी विचारधारा के अनुसार, साम्यवाद के सिद्धान्त तथा व्यवहार में इसके जन्म से ही शीत युद्ध के कीटाणु भरे हुए थे।
- साम्यवादी लेखकों के अनुसार शीत युद्ध का प्रमुख कारण अमेरिका की संसार पर प्रभाव जमाने की महत्त्वाकांक्षा में निहित है।
प्रश्न 4.
गुट-निरपेक्षता के कोई दो उद्देश्य लिखें।
उत्तर:
- गट-निरपेक्षता आन्दोलन का मख्य उद्देश्य सदस्य देशों को शक्ति गटों से अलग रखना था।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का उद्देश्य विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना था।
प्रश्न 5.
देतान्त से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
देतान्त (Detente) एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, शिथिलता अथवा तनाव शैथिल्य। जिन राज्यों में पहले तनावयुक्त स्पर्धा, ईर्ष्या तथा विरोध के सम्बन्ध रहे हों, उनमें इस प्रकार के सम्बन्धों के स्थान पर मित्रतापूर्वक सम्बन्धों का स्थापित हो जाना। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में देतान्त शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो महान् शक्तियों अर्थात् रूस तथा अमेरिका के सन्दर्भ में किया जाता है।
प्रश्न 6.
किसी एक परमाणु युद्ध की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
विश्व में अब तक केवल एक बार परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था। अगस्त, 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान के दो शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराये थे। इन बमों से इन दोनों शहरों को अत्यधिक हानि हुई। सैंकड़ों लोग मारे गए एवं लाखों लोग घायल एवं अपाहिज हो गए। इस परमाणु युद्ध का प्रभाव जापान के दोनों शहरों तथा लोगों पर आज भी देखा जा सकता है। इस घटना के तुरन्त बाद जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
प्रश्न 7.
द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह में शामिल किन्हीं चार देशों के नाम लिखिए।
उत्तर:
- इंग्लैंड,
- फ्रांस,
- रूस,
- संयुक्त राज्य अमेरिका।
प्रश्न 8.
सोवियत संघ तथा अमेरिका के द्वारा परस्पर विरोधी दुष्प्रचार ने किस प्रकार शीत युद्ध को बढ़ावा दिया ?
उत्तर:
सोवियत संघ तथा अमेरिका के द्वारा परस्पर विरोधी दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। सभी समाचार-पत्रों प्रावदा तथा इजवेस्तिया इत्यादि ने अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान शुरू किया। इसमें आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किये गए। इसी तरह पश्चिमी देशों ने भी सोवियत संघ की आलोचना करते हुए सोवियत संघ को ‘गुण्डों का नीच गिरोह’ तक कहा। अमेरिकी समाचार-पत्रों ने आगे लिखा कि साम्यवाद के प्रसार से इसाई सभ्यता को डूबने का खतरा है। इस प्रकार के लेखों ने शीत युद्ध को और अधिक बढ़ावा दिया।
प्रश्न 9.
अपरोध का क्या अर्थ है ?
उत्तर:
परमाणु युद्ध होने की स्थिति में विजेता का निर्णय करना असम्भव हो जाता है। यदि एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने का प्रयास करता है, तब भी विरोधी गुट के पास इतने परमाणु हथियार बचे रहते हैं, जिससे वह विरोधी देश पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति को अपरोध की स्थिति कहते हैं।
प्रश्न 10.
गुट-निरपेक्षता का अर्थ बताएं।
अथवा
गुट-निरपेक्षता का क्या अर्थ है ?
उत्तर:
गुट-निरपेक्षता का अर्थ है, किसी शक्ति गुट में शामिल न होना और शक्ति गुटों से सैनिक बन्धनों व अन्य सन्धियों से दूर रहना। गुट-निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है। गुट-निरपेक्षता का अर्थ बराबर दूरी भी नहीं है, क्योंकि गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उस देश या गुट का पक्ष लेते हैं, जो सही हो।।
प्रश्न 11.
बांडुंग सम्मेलन (1955) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर:
अप्रैल, 1955 में बांडंग स्थान में एशिया और अफ्रीकी राष्टों का एक सम्मेलन हआ जिसमें 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार करने के साथ साथ इनका विस्तार भी किया, अर्थात् पांच सिद्धान्तों के स्थान पर दस सिद्धान्तों की स्थापना की गई।
इस सम्मेलन में एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया तथा महान् शक्तियों का अनावश्यक अनुसरण न करने पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में सभी राज्यों की पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने, किसी राज्य पर सैनिक आक्रमण न करने तथा किसी राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर बल दिया गया।
प्रश्न 12.
बेलग्रेड शिखर सम्मेलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 एशियाई तथा अफ्रीकी व एक यूरोपियन राष्ट्र ने भाग लिया। लैटिन अमेरिका के तीन राष्ट्रों ने पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में महाशक्तियों से अपील की गई कि वे विश्व शान्ति तथा निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करें।
विश्व के सभी भागों एवं रूपों में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद की घोर निन्दा की गई। बेलग्रेड सम्मेलन में 20 सूत्रीय घोषणा-पत्र को स्वीकार किया गया। इस घोषणा में कहा गया कि विकासशील राष्ट्र बिना किसी भय व बाधा के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को प्रेरित करें।
प्रश्न 13.
नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) का क्या अर्थ है ?
उत्तर:
नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं सम्बन्धी समझौते करना तथा पुरानी परम्परावादी उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करना। नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत, विकसित राष्ट्रों के लिए एक आचार-संहिता बना कर तथा कम विकसित राष्ट्रों के उचित अधिकारों को मानकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सबके लिए समान तथा न्यायपूर्ण बनाना है।
प्रश्न 14.
उत्तरी एटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो) से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
उत्तरी एटलांटिक सन्धि संगठन (नाटो) विश्व का एक महत्त्वपर्ण सैनिक संगठन है जिसका निर्माण 1949 युद्ध के दौरान किया गया था। नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा पश्चिमी जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था।
प्रश्न 15.
वारसा पैक्ट से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
वारसा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई, 1955 में बनाया गया क्षेत्रीय सैनिक गठबन्धन था। इस संगठन में सोवियत संघ, पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा रूमानिया जैसे साम्यवादी देश शामिल थे। सोवियत संघ इस संगठन का सर्वेसर्वा था। परन्तु शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही फरवरी, 1991 में वारसा पैक्ट भी समाप्त हो गया।
प्रश्न 16.
केन्द्रीय सन्धि संगठन (सैन्टो) से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
केन्द्रीय सन्धि संगठन आरम्भ में बगदाद समझौते (1955) के रूप में सामने आया जोकि तुर्की और इराक के बीच हुआ था। परन्तु 1959 में इराक इस सन्धि से अलग हो गया जिसके कारण इसका नाम बदलकर सैन्टो कर दिया गया। सैन्टो में ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका थे। इस सन्धि का निर्माण मुख्य रूप से सोवियत संघ के विरुद्ध ही किया गया था। परन्तु 1979 में यह संगठन समाप्त हो गया।
प्रश्न 17.
दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्धि संगठन (सीटो) का क्या अर्थ है ?
उत्तर:
दक्षिण-पूर्वी एशिया सन्धि संगठन (सीटो) की स्थापना 1954 में की गई। इस संगठन में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, थाइलैण्ड तथा अमेरिका शामिल थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकना था। परन्तु 1977 में यह संगठन समाप्त हो गया।
प्रश्न 18.
शीत युद्ध के उदाहरण सहित दो अखाड़ों का वर्णन करें।
उत्तर:
- अफ़गानिस्तान-शीत युद्ध का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अखाड़ा अफगानिस्तान रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र-शीत युद्ध का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अखाड़ा संयुक्त राष्ट्र रहा है।
प्रश्न 19.
गुट-निरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाले तीन मुख्य देशों और उनके नेताओं के नाम लिखिए।
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का जन्म शीत युद्ध के दौरान हुआ। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य भी स्वयं को शीत युद्ध से दूर रखना था। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक देश है। भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं० नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्त्र के तत्कालिक राष्ट्रपति जमाल नासिर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक हैं।
प्रश्न 20.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के कोई चार महत्त्व लिखें।
उत्तर:
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने सदस्य देशों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को बढावा दिया है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने उपनिवेशवाद को समाप्त करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने सदस्य देशों को शीत युद्ध से दूर रखा।
प्रश्न 21.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका की व्याख्या करें।
उत्तर:
- भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक देश है।
- भारत ने गुट-निरपेक्ष देशों को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया है।
- भारत की पहल पर अफ्रीका कोष कायम किया गया।
- भारत ने गुट-निरपेक्ष देशों का ध्यान निःशस्त्रीकरण की तरफ खींचा।

प्रश्न 22.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को आरम्भिक दौर में एक दिशा एवं आकार प्रदान करने में भारत की भूमिका की व्याख्या करें।
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को प्रारम्भिक दौर में एक दिशा एवं आकार प्रदान करने में भारत की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रही है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के उदय के समय इसकी संख्या केवल 25 थी, परन्तु भारत के प्रयासों से अब इसकी संख्या 120 हो गई है। इसी प्रकार 1955 में बांडुंग सम्मेलन तथा 1961 में हुए बेलग्रेड सम्मेलन में इस आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने में भारत ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रश्न 23.
उपनिवेशीकरण की समाप्ति एवं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विस्तार के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन एवं उपनिवेशीकरण की समाप्ति एक-दूसरे से सम्बन्धित है। जैसे-जैसे उपनिवेश समाप्त होते गए, वैसे-वैसे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का विस्तार होता गया। क्योंकि अधिकांश उपनिवेशी राज्य स्वतन्त्र होकर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होते गए। इसीलिए जहां 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में केवल 25 देश शामिल थे, वहीं 2019 में हुए अजरबैजान सम्मेलन में इनकी संख्या 120 थी।
प्रश्न 24.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रकृति की व्याख्या करें।
उत्तर:
गट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रकति अपने आप में अनोखी है। वास्तव में इस आन्दोलन की प्रकति विषमांग स्वरूप की रही है। उदाहरण के लिए इसमें विकासशील देशों की संख्या अधिक है, जबकि विकसित देशों की कम। गुट-निरपेक्ष देशों में वैचारिक समानता का भी अभाव है अर्थात् इस आन्दोलन में उदारवादी, साम्यवादी तथा सुधारवादी सभी प्रकार के देश शामिल हैं। इस आन्दोलन में भिन्न-भिन्न जातियों एवं क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
प्रश्न 25.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अन्तर्गत ‘अफ्रीकी सहायता कोष’ तथा ‘पृथ्वी संरक्षण कोष’ की स्थापना कब, कहां और किस देश की पहल पर हुई ?
उत्तर:
अफ्रीकी कोष की स्थापना भारत की पहल पर सन् 1986 में जिम्बाबवे की राजधानी हरारे में हुए 8वें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन में की गई जबकि ‘पृथ्वी संरक्षण कोष’ की भी स्थापना भारत की पहल पर ही 1989 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुए 9वें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन में की गई।
प्रश्न 26.
‘आंशिक परमाण प्रतिबन्ध सन्धि 1963’ के विषय में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर:
आंशिक परमाणु प्रतिबन्ध सन्धि 5 अगस्त, 1963 में की गई। इस सन्धि का प्रमुख उद्देश्य परमाणु परीक्षणों को नियन्त्रित करना था। इस सन्धि पर अमेरिका, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किये थे। यह सन्धि 10 अक्तूबर, 1963 को लागू हो गई। इस सन्धि के अन्तर्गत वायुमण्डल, पानी के अन्दर तथा बाहरी अन्तरिक्ष में परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।
प्रश्न 27.
स्टार्ट-II सन्धि की व्याख्या करें।
उत्तर:
स्टार्ट-II (Strategic Arms Reduction Treaty-II) अर्थात् सामाजिक अस्त्र न्यूनीकरण सन्धि पर 3 जनवरी, 1993 को अमेरिका एवं रूस ने हस्ताक्षर किए। इस सन्धि का मुख्य उद्देश्य खतरनाक हथियारों को नियन्त्रित करने एवं उनकी संख्या कम करने से है, ताकि जनसंहार को रोका जा सके।
प्रश्न 28.
1919 में सोवियत संघ के पतन के बाद भारत किन दो तरीकों से रूस से सम्बन्ध रखकर लाभान्वित हुआ ?
उत्तर:
- भारत रूस से भी उसी प्रकार सम्बन्ध बनाने में सफल रहा, जिस प्रकार सोवियत संघ के साथ थे।
- भारत को रूस के माध्यम से इससे अलग हुए गणराज्यों से भी सम्बन्ध बनाने में आसानी हुई।
प्रश्न 29.
निम्नलिखित में से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के दो संस्थापकों के नामों की पहचान करें
(क) यासर अराफात
(ख) नेलसन मंडेला
(ग) डॉ० सुकर्णो
(घ) मार्शल टीटो।
उत्तर:
(ग) डॉ० सुकर्णो,
(घ) मार्शल टीटो।
प्रश्न 30.
1945 से 1990 तक किन्हीं दो महत्त्वपूर्ण विश्व राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करें।
उत्तर:
- दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व राजनीति में अमेरिका एवं सोवियत संघ और अधिक मज़बूत होकर उभरे।
- इस समय दोनों गुटों से अलग रहने वाले देशों ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की शुरुआत की।
प्रश्न 31.
शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर कब पहुंचा ?
उत्तर:
शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर सन् 1962 में पहुंचा, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु प्रक्षेपास्त्र तैनात कर दिये थे। इसमें सोवियत संघ एवं अमेरिका में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई।
प्रश्न 32.
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति के कोई दो सिद्धान्त बताएं।
उत्तर:
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने विश्व में स्वतन्त्रता एवं समानता की रक्षा को उस समय उद्देश्य बनाया।
- अमेरिका की विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त विश्व में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था।
प्रश्न 33.
शीत युद्ध के युग में एक पूर्वी गठबन्धन और तीन पश्चिमी गठबन्धनों के नाम लिखिए।
उत्तर:
शीत युद्ध के युग में पूर्वी गठबन्धन द्वारा वारसा पैक्ट तथा पश्चिमी गठबन्धन द्वारा नाटो, सैन्टो तथा सीटो जैसे गठबन्धन बनाए।
प्रश्न 34.
शीत युद्ध के दायरे से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर:
शीत युद्ध के दायरों से हमारा अभिप्राय यह है कि विश्व के किन-किन क्षेत्र विशेष या देश विशेष के कारण शीत युद्ध बढ़ा अथवा शीत युद्ध का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक देखा गया। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दायरे में अफ़गानिस्तान को शामिल किया जा सकता है।
प्रश्न 35.
कोई दो कारण दीजिए कि छोटे देशों ने शीत युद्ध के युग की मैत्री सन्धियों में महाशक्तियों के साथ अपने-आप को क्यों जोड़ा ?
उत्तर:
- छोटे देश महाशक्तियों के साथ अपने निजी हितों की रक्षा के लिए जुड़े।
- छोटे देश महाशक्तियों के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रतिद्वन्द्वी, देश के विरुद्ध सुरक्षा, हथियार तथा आर्थिक सहायता मिलती थी।
प्रश्न 36.
गुट-निरपेक्षता के मुख्य उद्देश्य बताएं।
अथवा
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के कोई दो उद्देश्य लिखिये।
उत्तर:
- गुट-निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को शक्ति गुटों से अलग रखना था।
- गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का उद्देश्य विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाना था।
प्रश्न 37.
तृतीय विश्व के देशों द्वारा नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करने के कोई दो कारण लिखिये।
उत्तर:
- पूर्वी एवं दक्षिणी विश्व के देश अपनी आत्मनिर्भरता के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर थे।
- विश्व अर्थव्यवस्था पर विकसित देशों का एकाधिकार ।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
1. शीत युद्ध किन दो गुटों से सम्बन्धित था ?
(A) चीन-पाकिस्तान
(B) अमेरिका गुट-सोवियत गुट
(C) फ्रांस-ब्रिटेन
(D) जर्मनी-इटली।
उत्तर:
(B) अमेरिका गुट-सोवियत गुट।
2. निम्न में से शीत युद्ध का सही अर्थ क्या है ?
(A) अमेरिकी एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु सम्बन्ध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे।
(B) तानाशाही व्यवस्था
(C) लोकतान्त्रिक व्यवस्था
(D) दोनों में से कोई नहीं।
उत्तर:
(A) अमेरिकी एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त कटु सम्बन्ध जो तनाव, भय एवं ईर्ष्या पर आधारित थे।
3. अमेरिकन गुट ने किस सैनिक गठबन्धन का निर्माण किया ?
(A) नाटो
(B) सीटो
(C) सैन्टो
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
4. सोवियत गुट ने निर्माण किया
(A) नाटो
(B) सीटो
(C) वारसा पैक्ट
(D) सैन्टो।
उत्तर:
(C) वारसा पैक्ट।

5. भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आन्दोलन की शुरुआत की ?
(A) असहयोग आन्दोलन
(B) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन
(C) सविनय अवज्ञा आन्दोलन
(D) भारत छोड़ो आन्दोलन।
उत्तर:
(B) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन।
6. नाटो (NATO) सन्धि का निर्माण कब किया गया ?
(A) सन् 1945 में
(B) सन् 1947 में
(C) सन् 1949 में
(D) सन् 1951 में।
उत्तर:
(C) सन् 1949 में।
7. ‘वारसा संधि’ का निर्माण कब हुआ ?
(A) सन् 1955 में
(B) सन् 1950 में
(C) सन् 1952 में
(D) सन् 1954 में।
उत्तर:
(A) सन् 1955 में।
8. पूंजीवादी देश है
(A) अमेरिका
(B) फ्रांस
(C) इंग्लैंड
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
9. सोवियत गुट (साम्यवादी गुट) में कौन-सा देश शामिल था ?
(A) पोलैण्ड
(B) पूर्वी जर्मनी
(C) बुल्गारिया
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
10. क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ ?
(A) सन् 1959 में
(B) सन् 1961 में
(C) सन् 1962 में
(D) सन् 1965 में।
उत्तर:
(C) सन् 1962 में।
11. शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ ?
(A) प्रथम विश्व युद्ध के पहले
(B) प्रथम विश्व युद्ध के बाद
(C) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
(D) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बाद।
उत्तर:
(C) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
12. शीतयुद्ध निम्न में से किसी एक से सम्बन्धित हैं
(A) राजनीतिक अविश्वास से
(B) सैनिक प्रतिस्पर्धा से
(C) वैचारिक मतभेद से
(D) उपरोक्त तीनों से।
उत्तर:
(D) उपरोक्त तीनों से।
13. शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन-सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया ?
(A) एशिया
(B) दक्षिण अमेरिका
(C) यूरोप
(D) अफ्रीका।
उत्तर:
(C) यूरोप।
14. महाशक्तियों के लिए छोटे देश लाभदायक थे
(A) अपने भू-क्षेत्र के कारण
(B) तेल और खनिज के कारण
(C) सैनिक ठिकाने के कारण
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
15. द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ?
(A) सन् 1939 ई० में
(B) सन् 1941 ई० में
(C) सन् 1943 ई० में
(D) सन् 1945 ई० में।
उत्तर:
(D) सन् 1945 ई० में।
16. वारसा पैक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था ?
(A) 1982
(B) 1984
(C) 1991
(D) 1995.
उत्तर:
(C) 1991
17. पूंजीवादी गुट का नेता कौन था ?
(A) सोवियत संघ
(B) अमेरिका
(C) भारत
(D) चीन।
उत्तर:
(B) अमेरिका।
18. साम्यवादी गुट का नेता कौन था ?
(A) भारत
(B) अमेरिका
(C) चीन
(D) सोवियत संघ।
उत्तर:
(D) सोवियत संघ।
19. शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बँटा हुआ था ?
(A) दो गुटों में
(B) तीन गुटों में
(C) चार गुटों में
(D) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।
उत्तर:
(A) दो गुटों में।
20. क्यूबा का सम्बन्ध किस महाशक्ति से था ?
(A) सोवियत संघ
(B) अमेरिका
(C) जापान
(D) भारत।
उत्तर:
(A) सोवियत संघ।
21. शीत युद्ध का प्रारम्भ कब हुआ ?
(A) प्रथम विश्व युद्ध से पहले
(B) प्रथम विश्व युद्ध के बाद
(C) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
(D) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बाद।
उत्तर:
(C) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
22. अगस्त, 1945 में अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए ?
(A) हिरोशिमा एवं नागासाकी
(B) हिरोशिमा एवं टोक्यो
(C) क्योवे एवं नागासाकी
(D) टोक्यो एवं नागासाकी।
उत्तर:
(A) हिरोशिमा एवं नागासाकी।
23. गोर्बाचोव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने ?
(A) 1980
(B) 1982
(C) 1984
(D) 1985
उत्तर:
(D) 1985.
24. पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य बनी ‘बर्लिन की दीवार’ को कब गिराया गया ?
(A) सन् 1979 में
(B) सन् 1986 में
(C) सन् 1989 में
(D) सन् 1990 में।
उत्तर:
(C) सन् 1989 में।
25. जर्मनी का एकीकरण कब हुआ ?
(A) 1980 में
(B) 1990 में
(C) 1991 में
(D) 1995 में।
उत्तर:
(B) 1990 में।
26. सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था ?
(A) 1985
(B) 1999
(C) 1995
(D) 1991.
उत्तर:
(D) 1991.
27. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापक हैं ?
(A) पं० जवाहर लाल नेहरू
(B) जोसेफ ब्रॉज टीटो
(C) गमाल अब्दुल नासिर
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
28. पहला गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कहां हुआ था ?
(A) नई दिल्ली
(B) बेलग्रेड
(C) टोक्यो
(D) मास्को।
उत्तर:
(B) बेलग्रेड।
29. पहले गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में कितने देश शामिल हुए थे ?
(A) 20
(B) 25
(C) 30
(D) 35.
उत्तर:
(B) 25.
30. निम्नलिखित में से एक देश गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक देश है ?
(A) भारत
(B) पाकिस्तान
(C) नेपाल
(D) मालदीव।
उत्तर:
(A) भारत।
31. निम्न में से किस वर्ष बांडुंग सम्मेलन हुआ ?
(A) 1950
(B) 1952
(C) 1955
(D) 1960.
उत्तर:
(C) 1955.
32. अभी तक गुट-निरपेक्षता के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं ?
(A) 14
(B) 17
(C) 16
(D) 18.
उत्तर:
(D) 18.
33. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का 18वां सम्मेलन कब हुआ ?
(A) 2019
(B) 2004
(C) 2005
(D) 2006.
उत्तर:
(A) 2019.
34. पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ ?
(A) सन् 1990 में
(B) सन् 1991 में
(C) सन् 1992 में
(D) सन् 1993 में।
उत्तर:
(A) सन् 1990 में।
35. गुट निरपेक्ष देशों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है?
(A) 114
(B) 116
(C) 118
(D) 120.
उत्तर:
(D) 120.
36. निम्न एक शीत युद्ध का परिणाम है
(A) एक धुव्रीय व्यवस्था
(B) द्वि-धुव्रीय व्यवस्था
(C) बहु-धुव्रीय व्यवस्था
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं।
उत्तर:
(B) द्वि-धुव्रीय व्यवस्था।
37. शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक था
(A) नाटो का गठन
(B) वारसा पैक्ट का गठन
(C) सैन्टो का गठन
(D) बर्लिन की दीवार का गिरना।
उत्तर:
(D) बर्लिन की दीवार का गिरना।

38. नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आरम्भ कब हुआ ?
(A) 1970 के दशक में
(B) 1980 के दशक में
(C) 1990 के दशक में
(D) 2000 के दशक में।
उत्तर:
(A) 1970 के दशक में।
39. नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध किन देशों से है ?
(A) पूंजीवादी देशों से
(B) विकसित देशों से
(C) विकासशील देशों से
(D) साम्यवादी देशों से।
उत्तर:
(C) विकासशील देशों से।
40. नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य है ?
(A) विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना
(B) विकासशील देशों द्वारा तैयार माल के निर्णय को प्रोत्साहन देना
(C) विकसित एवं विकासशील देशों के बीच तकनीकी विकास के अन्तर को समाप्त करना
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(D) उपरोक्त सभी।
41. विकासशील तथा विकसित देशों के बीच पाये जाने वाले विवाद को किस नाम से जाना जाता है ?
(A) उत्तर-दक्षिण विवाद
(B) पूर्व-पश्चिम विवाद
(C) उत्तर-पश्चिम विवाद
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर:
(A) उत्तर-दक्षिण विवाद।
42. “शीतयुद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदण्ड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है।” यह कथन किसका है ?
(A) स्टालिन
(B) चर्चिल
(C) पं०. जवाहर लाल नेहरू
(D) माओ-त्से तुंग।
उत्तर:
(C) पं० जवाहर लाल नेहरू।
रिक्त स्थान भरें
(1) वारसा सन्धि का निर्माण सन् ………… में हुआ।
उत्तर:
(1) 1955,
(2) अभी तक गुट-निरपेक्ष देशों के …………. शिखर सम्मेलन हो चुके हैं।
उत्तर:
18,
(3) द्वितीय विश्व युद्ध सन् 1939 से सन् ………… की अवधि में हुआ।
उत्तर:
1945,
(4) सन् 1961 में गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन ……………. में हुआ।
उत्तर:
बेलग्रेड,
(5) ………….. संकट के समय शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था।
उत्तर:
क्यूबा प्रक्षेपास्त्र,
(6) …………… का परिणाम द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था थी।
उत्तर:
शीत युद्ध,
(7) क्यूबा मिसाइल संकट सन् ……………. में हुआ।
उत्तर:
1962
(8) …………. को शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है।
उत्तर:
क्यूबा मिसाइल संकट,
(9) यू-2; विमान जासूसी कांड का सम्बन्ध …………… से माना जाता है।
उत्तर:
शीत युद्ध।
एक शब्द/वाक्य में उत्तर दें
प्रश्न 1.
गुट-निरपेक्ष देशों का 16वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2012 में किस देश में हुआ ?
उत्तर:
तेहरान।
प्रश्न 2.
नाटो (NATO) सन्धि का निर्माण कब हुआ ?
उत्तर:
सन् 1949 में।
प्रश्न 3.
शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन-सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया ?
उत्तर:
यूरोप
प्रश्न 4.
भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आन्दोलन की शुरुआत की ?
उत्तर:
भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की शुरुआत की।
प्रश्न 5.
गुटं-निरपेक्षता का अर्थ लिखें।
उत्तर:
गुट-निरपेक्षता का अर्थ है किसी गुट में शामिल न होना और स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करना।
प्रश्न 6.
जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ?
उत्तर:
सन् 1990 में।
![]()
![]()
![]()
![]()