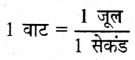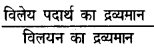HBSE 11th Class Physical Education Solutions Chapter 5 आसन
Haryana State Board HBSE 11th Class Physical Education Solutions Chapter 5 आसन Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 11th Class Physical Education Solutions Chapter 5 आसन
HBSE 11th Class Physical Education आसन Textbook Questions and Answers
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न (Long Answer Type Questions) |
प्रश्न 1.
अच्छे आसन की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालिए।
अथवा
संतुलित मुद्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तार से लिखें।
उत्तर:
आसन का मानवीय-जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। आसन से अभिप्राय शरीर की स्थिति से है अर्थात् मनुष्य किस प्रकार अपने शरीर की संभाल या देखरेख करता है। आसन की अवहेलना करना मानो कई प्रकार के शारीरिक दोषों या विकारों को निमंत्रित करना है। इसलिए बचपन से ही बच्चों के आसन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को शारीरिक विकारों से बचाया जा सके। एक अच्छा आसन ही मनुष्य की एक अच्छी शारीरिक संरचना या बनावट और विभिन्न स्थितियों में संतुलित रख सकता है। इसलिए शारीरिक संतुलन विभिन्न क्रियाओं; जैसे खड़े होना, बैठना, चलना, लेटना, पढ़ना आदि को करते हुए उचित होना चाहिए।
संतुलित आसन की अवस्थाएँ या स्थितियाँ (Positions of Correct Posture): उचित या अच्छे आसन की विभिन्न स्थितियाँ या अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं
1. खड़े रहने/होने का उचित आसन (Good Posture of Standing):
करूगर के अनुसार, “खड़े रहने का अच्छा आसन तभी कहा जा सकता है यदि खड़े रहते समय कम-से-कम शक्ति खर्च की जाए।” खड़े रहने या होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न आसनों का प्रयोग करते हैं। खड़े होने की उचित स्थिति हेतु व्यक्ति को अपने दोनों पैरों की एड़ियों को आपस में मिला लेना चाहिए। पैरों के अंगूठे आपस में 3 या 4 इंच की दूरी पर होने चाहिएँ। शरीर तना हुआ और शरीर का भार दोनों पैरों पर एक-समान या बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में व्यक्ति का संपूर्ण शरीर पूर्ण रूप से संतुलित होना चाहिए।
2. बैठने का उचित आसन (Good Posture of Sitting):
बहुत-से ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए हमें अधिक देर तक बैठना पड़ता है। अधिक देर बैठने से धड़ की माँसपेशियाँ थक जाती हैं और धड़ में कई दोष आ जाते हैं । बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती आमतौर पर खुली, कंधे समतल, पेट स्वाभाविक तौर पर अंदर की ओर, सिर और धड़ सीधी स्थिति में होने चाहिएँ। बैठने वाला स्थान हमेशा खुला, समतल तथा साफ-सुथरा होना चाहिए।
देखा जाता है कि कई व्यक्ति सही ढंग से बैठकर नहीं पढ़ते। पढ़ते समय मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिससे आँखों व शरीर पर कम-से-कम दबाव पड़े। लिखने के लिए मेज या डैस्क का झुकाव आगे की ओर होना चाहिए। हमें कभी भी सिर झुकाकर न तो पढ़ना चाहिए और न ही लिखना चाहिए। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गलत ढंग से बैठने से शरीर में कई विकार पैदा हो सकते हैं । बैठने के लिए व्यक्ति विभिन्न शारीरिक मुद्रा या आसन का प्रयोग करता है।
3. पढ़ने का उचित आसन (Good Posture of Reading):
व्यक्ति को इस प्रकार के आसन में बैठकर पढ़ना चाहिए, जिससे उसके शरीर तथा आँखों पर कम-से-कम दबाव पड़े। पढ़ते समय किताब से आँखों की दूरी उचित होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके, छोटे बच्चों की किताबें बड़े अक्षरों वाली होनी चाहिएँ, ताकि उनकी आँखों पर कम-से-कम दबाव पड़े तथा आँखें कमजोर न हो सकें। पढ़ते समय किताब इस प्रकार पकड़नी चाहिए जिससे उस पर रोशनी ठीक पड़ सके। आँखों के बिल्कुल समीप तथा बहुत दूर रखी हुई किताब कभी नहीं पढ़नी चाहिए।
4. चलने का उचित आसन (Good Posture of Walking):
चलने का आसन व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। चलते समय पैर समानांतर रखने चाहिएँ। सिर को सीधा रखना चाहिए तथा कंधे पीछे की तरफ होने चाहिएँ। छाती तनी हुई तथा बाजुएँ बिना किसी तनाव के झूलनी चाहिएँ। चलते समय पैर आपस में टकराने नहीं चाहिएँ तथा शरीर की माँसपेशियाँ साधारण स्थिति में होनी चाहिएँ। चलते समय ठीक आसन ही अपनाया जाना चाहिए ताकि शरीर में कम-से-कम थकावट हो सके। गलत आसन में चलने से शारीरिक ढाँचा ठीक नहीं रहता, क्योंकि इससे न सिर्फ टाँगें तथा माँसपेशियाँ थकती हैं, अपितु टाँगों तथा पैरों में दर्द भी होता रहता है।
5. लेटने या सोने का उचित आसन (Good Posture of Lying):
लेटते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि श्वसन क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। लेटते समय रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए। पीठ के बल अधिक समय तक नहीं लेटना चाहिए और न ही टाँगों को मोड़कर लेटना चाहिए, क्योंकि इससे साँस लेने में बाधा आती है। हमें नाक से ही साँस लेनी चाहिए। अत: माता-पिता को बच्चों के लेटने के आसन की ओर विशेष रूप से ध्यान देकर उन्हें उचित आसन हेतु प्रेरित करना चाहिए।
![]()
प्रश्न 2.
उचित आसन से आपका क्या अभिप्राय है? उचित आसन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए।
अथवा
उचित या संतुलित मुद्रा क्या है? इससे होने वाले लाभ बताएँ।
उत्तर:
उचित या अच्छे आसन का अर्थ (Meaning of Correct or Good Posture):
आसन या मुद्रा शरीर की स्थिति को कहते हैं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना आदि। अच्छे आसन से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर का ठीक या उचित संतुलन में होना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते समय उचित या अच्छा होना चाहिए। वास्तव में एक खड़े हुए व्यक्ति का उचित आसन उस अवस्था में होगा, जब उसके शरीर का भार उसके दोनों पैरों पर एक-समान होगा। एवेरी (Avery) के अनुसार, “एक अच्छा आसन वह है जिसमें शरीर संतुलित हो, जिससे कम-से-कम थकावट उत्पन्न हो।” अत: शरीर के विभिन्न अंगों की ठीक स्थिति को ही उचित आसन कहते हैं।
उचित या अच्छे आसन के लाभ (Advantages of Correct or Good Posture):
शरीर की किसी एक स्थिति को मुद्रा नहीं कहा जाता बल्कि हम अपने शरीर को कई अलग-अलग ढंगों से स्थिर करते रहते हैं। शरीर को स्थिर रखने की स्थितियों को मुद्रा या आसन कहा जाता है। शरीर की प्रत्येक प्रकार की स्थिति मुद्रा ही कहलाएगी। परंतु गलत और ठीक मुद्रा में बहुत अंतर होता है। ठीक मुद्रा देखने में सुंदर लगती है।
इससे शरीर की माँसपेशियों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। ठीक मुद्रा वाला व्यक्ति काम करने तथा चलने-फिरने में चुस्त और फुर्तीला होता है। गलत मुद्रा व्यक्ति के शरीर के लिए अनावश्यक बोझ बन जाती है। इसलिए हमेशा शरीर की स्थिति प्रत्येक प्रकार का आसन प्राप्त करते समय ठीक रखनी चाहिए। संक्षेप में, उचित या संतुलित मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं
- शरीर को उचित मुद्रा में रखने से शरीर को हिलाना-डुलाना आसान हो जाता है और शरीर के दूसरे भागों पर भी भार नहीं पड़ता।
- उचित मुद्रा मन को प्रसन्नता एवं खुशी प्रदान करती है।
- उचित मुद्रा वाले व्यक्ति की कार्य करने में कम शक्ति लगती है अर्थात् उसे कोई कार्य करने में कठिनाई नहीं होती।
- उचित मुद्रा हड्डियों और माँसपेशियों को संतुलित रखती है।
- उचित मुद्रा वाले व्यक्ति को बीमारियाँ कम लगती हैं।
- उचित आसन से व्यक्ति की शारीरिक आकृति आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देती है अर्थात् उसका शारीरिक ढाँचा बहुत आकर्षित दिखता है।
- इससे स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
- इससे शारीरिक योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि होती है।
- इससे व्यक्ति की भूख में वृद्धि होती है जिससे उसके शारीरिक व मानसिक विकास में वृद्धि होती है।
- यह अनेक प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में लगने वाली क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है।
- इससे व्यक्ति में आत्म-विश्वास की वृद्धि होती है। वह अपने विचारों या भावों को विश्वास के साथ व्यक्त करता है।
- इससे रीढ़ की हड्डियों में लचकता आती है।
- इससे शरीर में स्फूर्ति एवं उमंग बढ़ती है।
- इससे शरीर के सभी अंगों का उचित विकास होता है, क्योंकि इससे शारीरिक विकार दूर होते हैं।
- इससे मन की तत्परता का पता चलता है अर्थात् यह मानसिक या बौद्धिक विकास में सहायक होता है।
- अच्छे आसन से व्यक्तित्व आकर्षण लगता है। यह व्यक्ति के सम्मान और नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक होता है।
- अच्छी मुद्रा या आसन से माँसपेशी, श्वसन, पाचन एवं नाड़ी आदि संस्थानों की क्षमता में सुधार होता है और आपसी तालमेल भी बढ़ता है। इससे शरीर के सभी संस्थान सुचारु रूप से कार्य करते हैं।
- अच्छे आसन से विभिन्न प्रकार के कौशलों की संपूर्णता में सुधार होता है।
- अच्छे आसन से शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं में सुधार होता है और मन की तत्परता व शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है।
- अच्छे आसन से समाजीकरण की योग्यता का पता चलता है। यह व्यक्ति के समाज में उच्च-स्तर का द्योतक है।
प्रश्न 3.
मुद्रा की किस्मों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दीजिए।
उत्तर:
मुद्रा या आसन की किस्में निम्नलिखित हैं
1. स्थैतिक मुद्रा (Static Posture):
जिस मुद्रा में शरीर की स्थिति स्थिर रहती है, उसे स्थैतिक मुद्रा कहते हैं; जैसे खड़े होने की मुद्रा, बैठने की मुद्रा तथा लेटने की मुद्रा।
(i) खड़े होने की मुद्रा (Posture of Standing):
गलत ढंग से खड़े होने अथवा चलने से भी शरीर में थकावट आ जाती है। खड़े होने के दौरान शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए। खड़े होने के दौरान पेट सीधा, छाती फैली हुई और धड़ सीधा होना चाहिए।
(ii) बैठने की मुद्रा (Posture of Sitting):
बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती आमतौर पर खुली, कंधे समतल, पेट स्वाभाविक तौर पर अंदर की ओर, सिर और धड़ सीधी स्थिति में होने चाहिए। बैठने वाला स्थान हमेशा खुला और समतल होना चाहिए। देखा जाता है कि कई व्यक्ति सही ढंग से बैठकर नहीं पढ़ते । पढ़ते समय हमें ऐसी मुद्रा में बैठना चाहिए जिससे आँखों व शरीर पर कम-से-कम दबाव पड़े। हमें कभी भी सिर झुकाकर न तो पढ़ना चाहिए और न ही लिखना चाहिए। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
(iii) लेटने की मुद्रा (Posture of Lying):
लेटते समय हमारा शरीर विश्राम अवस्था में और शांत होना चाहिए। सोते समय शरीर प्राकृतिक तौर पर टिका होना चाहिए। हमें सोते समय कभी भी गलत तरीके से नहीं लेटना चाहिए। इससे हमारे रक्त के संचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे श्वास क्रिया भी रुक जाने का खतरा पैदा हो सकता है। गर्दन अथवा अन्य किसी भाग की नाड़ी आदि चढ़ जाने का खतरा रहता है।
2. गतिज मुद्रा (Kinetic Posture):
जिस मुद्रा में शरीर की स्थिति गतिशील अवस्था में होती है, उसे गतिज मुद्रा कहते हैं; जैसे चलने की मुद्रा । हमारी चाल हमेशा सही होनी चाहिए। चलते समय पंजे और एड़ियों पर ठीक भार पड़ना चाहिए। अच्छी चाल वाला व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलते समय पैरों का अंतर समान रहना चाहिए। हाथ आगे-पीछे आने-जाने चाहिएँ। चलते समय पैरों की रेखाएँ चलने की दिशा की रेखा के समान होनी चाहिएँ।।
3. उचित मुद्रा (Correct Posture):
आसन या मुद्रा शरीर की स्थिति को कहते हैं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना आदि। अच्छे आसन से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर का ठीक एवं उचित संतुलन में होना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते हुए उचित या अच्छा होना चाहिए। वास्तव में एक खड़े हुए व्यक्ति का उचित आसन उस अवस्था में होगा, जब उसके शरीर का भार उसके दोनों पैरों पर एक-समान होगा।
4. अनुचित मुद्रा (Incorrect Posture):
भद्दी मुद्रा या अनुचित आसन मनुष्य के व्यक्तित्व में बाधा डालता है, जिसके कारण मनुष्य में आत्म-विश्वास की कमी आ जाती है। शरीर की स्थिति ठीक अवस्था में न होना अनुचित आसन कहलाता है अर्थात् चलते, बैठते, लिखते, पढ़ते व खड़े होते समय शरीर का उचित अवस्था या स्थिति में न रहना अनुचित आसन कहलाता है।
प्रश्न 4.
आसन संबंधी विकृतियों से आप क्या समझते हैं? आसन संबंधी विकृतियों के कारणों का वर्णन कीजिए।
अथवा
आसन संबंधी कुरूपताओं से आपका क्या तात्पर्य है? इनके कारणों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
आसन संबंधी कुरूपताओं का अर्थ (Meaning of Postural Deformities):
आसन संबंधी कुरूपताओं या विकृतियों से अभिप्राय शरीर की स्थिति का ठीक या संतुलन अवस्था में न होना है। ऐसी स्थिति से शरीर को अनेक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। यदि इनको समय रहते ठीक न किया जाए तो इनका हमारे शारीरिक विकास एवं वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
आसन संबंधी कुरूपताओं या विकृतियों के कारण (Causes of Postural Deformities): आसन संबंधी कुरूपताओं के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं
1.पैदा होते समय कुरूपता (Inborn Deformity):
कुछ आसन पैदा होने के समय कुरूपता वाले होते हैं । इसका मुख्य कारण संतुलित भोजन न होना अथवा पैदा होने से पहले अधिक ध्यान न देना है। इस प्रकार की कुरूपताएँ स्थायी होती हैं।
2. कमजोर हड्डियाँ तथा माँसपेशियाँ (Weak Bones and Muscles):
आसन में कुरूपता का मुख्य कारण कमजोर हड्डियाँ और माँसपेशियाँ हैं। विटामिन ‘डी’ की कमी के कारण मनुष्य की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। जिसके कारण वे मुड़ जाती हैं। मनुष्य के शरीर में माँसपेशियाँ लीवर का कार्य करती हैं, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। इनमें दोष पड़ने से रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, पीछे की तरफ कूब, आगे की तरफ कूब जैसी कुरूपताएँ पैदा हो जाती हैं।
3. बुरी आदतें (Bad Habits):
बैठते, उठते, लेटते समय, खड़े होते समय तथा कार्य करते समय गलत आसन शरीर में कुरूपताएँ पैदा करते हैं। उदाहरणस्वरूप पढ़ते समय हम एक तरफ झुककर अथवा कुर्सी पर बैठकर, मेज पर झुककर पढ़ते हैं, फिर यह आदत बन जाती है, जिससे आसन में कुरूपता आ जाती है।
4. अधिक दबाव (High Pressure):
अधिक दबाव के कारण भी शरीर में कुरूपताएँ आ जाती हैं। विशेषतौर पर बाल्यावस्था में माँसपेशियों तथा हड्डियों में अधिक दबाव हानिकारक होता है।
5. शरीर का अधिक भारी होना या मोटापा (Heavy Body or Obesity):
अधिक भारी शरीर हड्डियों, माँसपेशियों तथा लिगामेंट्स पर अधिक भार डालता है जिसके कारण आगे की ओर कूब (Lordosis), बाहर की तरफ मुड़ी हुई टाँगें (Bow Legs) तथा चपटे पैर (Flat Feet) जैसी कुरूपताएँ आ जाती हैं। अधिक भार से घुटने के जोड़ों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
6. व्यायाम की कमी (Lack of Exercise):
आसन संबंधी कुरूपताएँ आने का सबसे बड़ा कारण व्यायाम की कमी है, क्योंकि व्यायाम हमारी माँसपेशियों में शक्ति तथा नीरोगता लाते हैं। जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम नहीं करते, उनकी माँसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें कई बार स्थायी तौर पर कुरूपताएँ आ जाती हैं। बच्चे के लिए ठीक व्यायाम उसके आसन को सुंदरता प्रदान करते हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व में वृद्धि होती है।
7. असुविधाजनक वस्त्र (Uncomfortable Clothes):
कई बार असुविधाजनक वस्त्र शरीर को गलत आसन हेतु मजबूर कर देते हैं, विशेषतौर पर तंग वस्त्र । तंग वस्त्र शरीर की हरकतों, माँसपेशियों तथा जोड़ों की गतिशीलता में बाधा पैदा करते हैं।
8. बीमारी अथवा दुर्घटना (Disease or Accident):
बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण भी आसन में कुरूपताएँ आ जाती हैं। दुर्घटना के कारण आसन में आई कुरूपता डॉक्टर की सलाह से दूर की जा सकती है, परंतु कई बार दुर्घटना से आसन में स्थायी तौर पर कुरूपता आ जाती है। बीमारी के कारण बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने से भी माँसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण कुरूपता आ जाती है।
9. मनोवैज्ञानिक तनाव (Psychological Tension):
मनोवैज्ञानिक तनाव या चिंता से भावनात्मक स्थिति में असंतुलन पैदा होता है जिससे हमारे आसन में कुरूपता आ जाती है।
10. असंतुलित आहार (Unbalanced Diet):
असंतुलित या पोषक तत्त्वहीन आहार से शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसके कारण भी आसन की अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
![]()
प्रश्न 5.
रीढ़ की हड्डी का पीछे की तरफ कूब या कूबड़ होने के कारणों तथा इसको ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
पीछे के कूब (कूबड़) जैसी कुरूपता का मुख्य कारण रीढ़ की हड्डी का पीछे की तरफ झुक जाना है। इसमें गर्दन अगली तरफ झुक जाती है तथा पीठ वाला हिस्सा पिछली तरफ झुक जाता है। रीढ़ की हड्डी एक कमान जैसा रूप धारण कर लेती है। रीढ़ की हड्डी में कुरूपता पीठ की माँसपेशियों के सिकुड़ने से होती है।
कारण (Causes): रीढ़ की हड्डी का पीछे की तरफ कूब (काइफोसिस) होने के कारण निम्नलिखित हैं
- आगे की ओर झुककर पढ़ने तथा काम करने से।
- व्यायाम की कमी के कारण।
- लंबा कद होने के कारण।
- बीमारी अथवा दुर्घटना होने के कारण।
- बैठने के लिए अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करने के कारण।
- शारीरिक कमजोरी व विकार के कारण।
- लंबे समय तक अनुचित मुद्रा में बैठने के कारण आदि।
ठीक करने के उपाय (Remedial Measures):
रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ कूब होने की विकृति को निम्नलिखित उपायों द्वारा ठीक किया जा सकता है
- पीछे की तरफ कूब को ठीक करने के लिए नियमित व्यायाम करने चाहिएँ।व्यायाम करने से इस स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने लगता है।
- पीठ की माँसपेशियों को शक्तिशाली बनाने वाले व्यायाम करने चाहिएँ।
- लंबे-लंबे साँस लेने वाले व्यायाम करने चाहिएँ।
- छाती को आगे की तरफ सीधा करके चलना-फिरना चाहिए।
- लटकने वाले व्यायाम करने चाहिएँ।
- कुर्सी पर बैठते समय आसन को आगे की तरफ खींचकर बैठना चाहिए।
- इसको ठीक करने के लिए योग-आसन काफी लाभदायक हैं; जैसे भुजंगासन, शलभासन, सर्वांगासन तथा चक्रासन आदि।
- सोते समय अपनी पीठ के नीचे तकिया अवश्य रखें। ऐसा करके भी इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है।
प्रश्न 6.
रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ कूब या कूबड़ होने के कारणों तथा इसको ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
आगे की तरफ कूब का भी मुख्य कारण अच्छा आसन धारण न करना है। इसमें रीढ़ की हड्डी ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे पेट के पास आगे की ओर झुकी होती है। छाती आगे की तरफ तथा गर्दन पिछली तरफ झुक जाती है। यह कुरूपता काफी दुखदायी है, क्योंकि इससे चलने-फिरने, उठने-बैठने में काफी मुश्किलें आती हैं। इससे छाती तथा गर्दन की माँसपेशियों में अकड़ाव आ जाता है और कूल्हे की माँसपेशियाँ छोटी और पेट की माँसपेशियाँ लंबी हो जाती हैं।
कारण (Causes): रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ कूब या लॉर्डोसिस होने के कारण निम्नलिखित हैं
- व्यायाम की कमी के कारण।
- छाती तथा गर्दन की कमजोर माँसपेशियों के कारण।
- संतुलित भोजन की कमी के कारण।
- गलत आसन धारण करने के कारण।
ठीक करने के उपाय (Remedial Measures): रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ कूब को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- पीठ के बल लेटने वाले व्यायाम करना।
- खड़े होकर धड़ को अगली तरफ झुकाना।
- गर्दन तथा कंधों को आगे की ओर झुकाकर लंबे-लंबे साँस लेना।
- पैरों को जोड़कर हाथों से पैरों को छूना
- इसको ठीक करने के लिए योग-आसन काफी लाभदायक है; जैसे हलासन तथा पद्मासन।
प्रश्न 7.
रीढ़ की हड्डी के एक ओर झुकने के क्या कारण हैं? इसको दूर करने के उपाय बताएँ।
अथवा
स्कोलिओसिस (Scoliosis) क्या है? इसको ठीक करने के उपायों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुकना (Scoliosis or Spinal Deviation): रीढ़ की हड्डी का शरीर के दाईं या बाईं ओर झुकना या मुड़ना स्कोलिओसिस (Scoliosis) कहलाता है। स्कोलिओसिस का अर्थ है-झुकना, मुड़ना, ऐंठना या घुमना। वास्तव में इसमें बराबर की ओर एक गोलाई वक्र होता है जो स्कोलिओटिक वक्र (Scoliotic Curve) कहलाता है। जब यह वक्र रीढ़ की हड्डियों के बाईं ओर हो तो यह सामान्यतया ‘C’ वक्र कहलाता है। कई बार यह वक्र दोनों ओर भी हो सकता है, तब यह ‘S’ वक्र कहलाता है, क्योंकि उस समय आकृति ‘S’ के आकार जैसी हो जाती है। ठीक से न बैठने, चलने व खड़े होने से यह विकृति हो जाती है। परन्तु रीढ़ की हड्डी के मुड़ने का मुख्य कारण रिकेट्स व पोलियो जैसी बीमारियाँ हैं।
कारण (Causes): रीढ़ की हड्डी के एक ओर झुकने के कारण निम्नलिखित हैं
- हड्डियों के जोड़ों से संबंधित बीमारी होने के कारण।
- भोजन में आवश्यक तत्त्वों की कमी होने के कारण।
- उचित आसन धारण न करने के कारण।
- टाँगों के विकसित न होने के कारण।
- रिकेट्स व पोलियो रोग हो जाने के कारण।
- माँसपेशियों के कमजोर होने के कारण।
ठीक करने के उपाय (Remedial Measures): स्कोलिओसिस को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- उचित आसन धारण करना।
- पढ़ाई करते समय झुकने वाली अवस्था से बचना।
- हॉरिजौंटल बार को दोनों हाथों से पकड़कर शरीर को दाईं और बाईं ओर झुकाना।
- तैरने की ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक का प्रयोग करके तैरना।
प्रश्न 8.
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें
(क) गोल या झुके हुए कंधे (Round Shoulders)
(ख) घुटनों का आपस में टकराना या भिड़ना (Knock Knees)।
उत्तर:
(क) गोल या झुके हुए कंधे के कारण (Causes of Round Shoulders): आसन संबंधी गोल या झुके हुए कंधे की विकृति के कारण अग्रलिखित हैं
- आनुवांशिकता संबंधी दोष।
- उचित आसन धारण न करना अर्थात् झुकी हुई अवस्था में बैठना, खड़े होना आदि।
- व्यायाम न करना।
- अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करने के कारण।
ठीक करने के उपाय (Remedial Measures): गोल या झुके हुए कंधे की विकृति को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- कुछ समय तक हॉरिजौटल बार पर लटकना।
- नियमित रूप से व्यायाम व आसन करना, विशेषकर धनुरासन व चक्रासन।
- अपनी कोहनियों को वृत्ताकार रूप से बारी-बारी से विपरीत दिशा में घुमाना।
(ख) घुटनों का आपस में टकराना या भिड़ना (Knock Knees):
इस कुरूपता में दोनों घुटने आपस में मिल जाते हैं। जब बच्चा खड़ा होता है तो पाँव समानांतर रहते हैं। टखनों के मध्य का स्थान अधिक हो जाता है। बच्चा चलने तथा दौड़ने में कठिनाई महसूस करता है। वह अपनी सामान्य प्रसन्नता खो देता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों पाँवों को सटाकर सीधा खड़ा होता है तब एक सामान्य आसन के दौरान घुटनों में थोड़ा अंतर होना चाहिए। अगर अंतर ज्यादा है और घुटने आपस में स्पर्श करते हैं तो इस कुरूपता को घुटनों का आपस में भिड़ना कहते हैं।
कारण (Causes): छोटे बच्चों के भोजन में कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन ‘डी’ की कमी के कारण उनकी हड्डियाँ कमजोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं । इस कारण उनके घुटने टकराने लग जाते हैं । इस स्थिति में उन बच्चों से सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं हुआ जाता। उनके पाँव जुड़ने से पहले ही उसके घुटने टकराने लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अच्छी तरह से भागना तथा चलना मुश्किल हो जाता है।
ठीक करने के उपाय (Remedial Measures): घुटनों के आपस में टकराने को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
(1) इस कुरूपता को दूर करने के लिए टाँगों की ऐसी कसरतें करवानी चाहिएँ, जिनसे घुटनों को बाहर निकाला जा सके।
(2) इस कुरूपता को ठीक करने के लिए साइकिल चलानी चाहिए।
(3) इस कुरूपता के लिए तैराकी और घुड़सवारी लाभदायक है।
(4) नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन करना चाहिए।
(5) कैल्शियम व फॉस्फोरस तथा विटामिन ‘डी’ युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए।
प्रश्न 9.
आसन संबंधी चपटे पैर की विकृति के कारणों तथा इसको ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
चपटे पैरों की विकृति प्रायः बच्चों तथा वृद्धों में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण बच्चे द्वारा गलत आसन धारण करना है। इससे पैरों की हड्डियों की बनावट में अंतर आता है तथा पैर का निचला हिस्सा नीचे की ओर झुक जाता है।
- कारण (Causes): चपटे पैरों की विकृति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं
- पैरों की कमजोर माँसपेशियाँ।
- अधिक वजन उठाना।
- लंबे समय तक जूतों का प्रयोग किए बिना खड़े रहना।
- मोटापा।
- पुरानी बीमारी।
- लक्षण (Symptoms): चपटे पैरों के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं
- पैरों में कमजोरी होना।
- घुटने व पीठ की माँसपेशियों में दर्द होना।
- चलने में कठिनाई आना।
- पैरों में अधिक पसीने का आना।
- पैरों का सुन्न रहना।
- पैरों में भौरियों का निकलना।
- ठीक करने के उपाय (Remedial Measures): चपटे पैरों को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- पैरों में फिट आने वाले जूते पहनने चाहिएँ।
- चलते समय पैरों के बाहरी तरफ अधिक वजन डालना चाहिए।
- एक अवस्था में लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना चाहिए।
- पंजों के बल दौड़ना व साइकिल चलानी चाहिए।
- पैरों को इकट्ठा करके पंजों के बल बैठना चाहिए।
- पंजों पर वजन उठाकर व्यायाम करना चाहिए।
- इस विकृति को ठीक करने में घुड़दौड़ काफी लाभदायक है।
![]()
प्रश्न 10.
आसन संबंधी कुरूपताओं या विकृतियों में सुधार हेतु लाभदायक व्यायामों या शारीरिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
प्लेटो (Plato) के अनुसार, “गतिविधि या व्यायाम का अभाव प्रत्येक इंसान की अच्छी स्थिति को नष्ट कर देता है, जबकि व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम इसे बचाए और बनाए रखते हैं।” बहुत-सी ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या व्यायाम होते हैं जिनको आसन संबंधी विकृतियों या विकारों को सामान्य करने के लिए सुधारात्मक उपायों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है; जैसे
1. पीछे की ओर कूब या काइफोसिस (Kyphosis): इस विकृति में सुधार हेतु लाभदायक व्यायाम या क्रियाएँ निम्नलिखित हैं
(i) पीठ के बल लेटकर घुटनों को ऊपर की ओर उठाएँ और पैरों के तलवे जमीन को स्पर्श न करें। इसके बाद हॉरिजौटल अवस्था में दोनों हाथों को बराबर खोलकर सिर के ऊपर ले जाएँ। हथेलियाँ ऊपर की ओर होनी चाहिए। इस अवस्था में कुछ देर तक रहें। इसके बाद अपने हाथों को हॉरिजौंटल अवस्था में लाएँ। इस प्रकार से यह क्रिया 7-8 बार दोहरानी चाहिए।
(ii) छाती के बल लेटकर हाथों को अपने कूल्हों पर रखें। इसके बाद अपने सिर एवं धड़ को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाएँ। इस अवस्था में कुछ समय तक रुककर अपनी पहले वाली अवस्था में आएँ। इस प्रकार से यह क्रिया कई बार दोहरानी चाहिए।
2. आगे की ओर कूब या लॉर्डोसिस (Lordosis): इस विकृति में सुधार हेतु लाभदायक व्यायाम या क्रियाएँ निम्नलिखित हैं
(i) छाती के बल लेटकर अपने दोनों हाथ उदर पर रखें। इसके बाद कूल्हों एवं कंधों को नीचे रखें। फिर पीठ के निचले भाग को उठाने का प्रयास करें। इस प्रकार से यह क्रिया 5-6 बार दोहराएँ।
(ii) फर्श पर अधोमुख अवस्था में लेटकर अपने कंधों की चौड़ाई के अनुसार अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ फर्श पर रखें। श्रोणी (Pelvis) को फर्श पर रखते हुए धड़ को ऊपर की ओर ले जाएँ। इस अवस्था में कुछ देर तक रहने के बाद पहले वाली अवस्था में आ जाएँ। इस प्रकार से यह प्रक्रिया कई बार दोहराएँ।
3. रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुकाव या स्कोलिओसिस (Scoliosis): इस विकृति में सुधार हेतु लाभदायक व्यायाम या क्रियाएँ निम्नलिखित हैं
(i) छाती के बल लेटकर अपनी दाईं बाजू को ऊपर और बाईं बाजू को बराबर में रखें। इसके बाद दाईं बाज को सिर के ऊपर से बाईं ओर ले जाकर बाएँ हाथ से दबाएँ और कूल्हे को थोड़ा ऊपर की ओर सरकाएँ। इस प्रकार यह प्रक्रिया इस विकार में सुधार करने में सहायक होती है।
(ii) पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएँ। इसके बाद एड़ी एवं कूल्हे को ऊपर उठाकर अपनी दाईं बाजू को चाप के रूप में सिर के ऊपर से बाईं ओर ले जाएँ। फिर बाएँ हाथ से बाईं ओर की पसलियों या रिब्स को दबाएँ।
4. चपटे पैर (Flat Foot): इस विकृति में सुधार हेतु लाभदायक व्यायाम या क्रियाएँ निम्नलिखित हैं
- पैरों को इकट्ठा करके पंजों के बल बैठना।
- सीधे खड़े होकर एड़ियों को ऊपर व नीचे करना।
- नियमित रूप से रस्सी कूदना।
- नियमित रूप से पंजों पर वजन उठाकर व्यायाम करना।
5. घुटनों का आपस में टकराना (Knock-Knee): इस विकृति में सुधार हेतु लाभदायक व्यायाम या क्रियाएँ निम्नलिखित हैं
- घुड़सवारी करना और साइकिल चलाना।
- नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन करना।
6. गोल कंधे (Round Shoulders): इस विकृति में सुधार हेतु लाभदायक व्यायाम या क्रियाएँ निम्नलिखित हैं
- नियमित रूप से हॉरिजौटल बार पर कुछ समय के लिए लटकना।
- नियमित रूप से चक्रासन एवं धनुरासन करना।।
- अपनी कोहनियों को कुछ समय तक घड़ी की सूई की दिशा में और कुछ समय घड़ी की सूई की विपरीत दिशा में वृत्ताकार रूप से घूमना।
प्रश्न 11.
भद्दी मुद्रा से क्या अभिप्राय है? इसके कारणों तथा इसको दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए।
अथवा
अनुचित आसन क्या है? इसको ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा आसन की खराबी को कैसे दूर करेंगे?
उत्तर:
अनुचित आसन का अर्थ (Meaning of Incorrect Posture): भद्दी मुद्रा या अनुचित आसन मनुष्य के व्यक्तित्व में बाधा डालता है, जिसके कारण मनुष्य में आत्म-विश्वास की कमी आ जाती है। शरीर की स्थिति ठीक अवस्था में न होना अनुचित आसन कहलाता है अर्थात् चलते, बैठते, लिखते, पढ़ते व खड़े होते समय शरीर का उचित अवस्था या स्थिति में न रहना अनुचित आसन कहलाता है।
अनुचित या भद्दी मुद्रा या आसन के कारण (Causes of Incorrect or Bad Posture): इस आसन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं
1. संतुलित व पौष्टिक आहार (Balanced and Nutritious Food):
शरीर की बनावट के लिए संतुलित व पौष्टिक आहार का होना बहुत जरूरी है। इसकी कमी के कारण शारीरिक अंगों का विकास रुक जाता है। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक ढाँचा कमजोर पड़ जाता है जिसके कारण आसन में कुरूपता आ जाती है।
2. व्यायामों की कमी (Lack of Exercises):
व्यायामों की कमी के कारण शरीर की माँसपेशियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे आसन बेढंगा हो जाता है। व्यायाम अच्छे आसन के लिए लाभदायक होते हैं।
3. शरीर का अधिक भार (Over Weight of Body):
शरीर का अधिक भारी होना भी भद्दी मुद्रा का कारण है। मोटापे के कारण व्यक्ति को चलने-फिरने में कठिनाई महसूस होती है। इसका उसके आसन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4. बुरी आदतें (Bad Habits):
गलत ढंग से पढ़ने, लिखने, बैठने, खड़े होने तथा चलने वाली बुरी आदतें मनुष्य के आसन में कुरूपता लाती हैं।
5. असुविधाजनक वस्त्र (Uncomfortable Clothes):
तंग वस्त्र, जूते, पैंट-कमीज आदि डालने से शरीर में तनाव बना रहता है, जिससे मनुष्य आराम महसूस नहीं करता। इससे वह बुरा आसन ग्रहण करता है।
भद्दी मुद्रा को ठीक करने के उपाय (Remedial Measures for Bad Posture): भद्दी या अनुचित आसन को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- बच्चों को ठीक मुद्रा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। स्कूल में अध्यापकों और घर में माता-पिता का कर्तव्य है कि बच्चों की खराब मुद्रा को ठीक करने के लिए निरंतर प्रयास करें।
- भोजन की कमी के कारण आई कमजोरी को ठीक करना चाहिए।
- बच्चों को न तो तंग कपड़े डालने चाहिएँ और न ही तंग जूते।
- हमें गलत ढंग से न तो चलना चाहिए और न ही पढ़ना व बैठना चाहिए।
- उचित और पूरी नींद लेनी चाहिए।
- बच्चों के स्कूल बैग का भार हल्का होना चाहिए।
- आवश्यकतानुसार डॉक्टरी परीक्षण करवाते रहना चाहिए ताकि मुद्रा-त्रुटि को समय पर ठीक किया जा सके।
- हमारे घरों, स्कूलों और कॉलेजों में ठीक मुद्रा की जानकारी देने वाले चित्र लगे होने चाहिएँ।
- घरों और स्कूलों में बड़ा शीशा लगा होना चाहिए, जिसके आगे खड़े होकर बच्चा अपनी मुद्रा देख सके।
- सोते समय शरीर को अधिक नहीं मोड़ना चाहिए।
- संतुलित एवं पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए।
- बुरी आदतों से बचना चाहिए।
- नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए।
लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)
प्रश्न 1.
आसन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
आसन का मानवीय-जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। आसन से अभिप्राय शरीर की स्थिति से है अर्थात् मनुष्य किस प्रकार अपने शरीर की संभाल या देखरेख करता है। आसन की अवहेलना करना मानो कई प्रकार के शारीरिक दोषों या विकारों को निमंत्रित करना है। इसलिए बचपन से ही बच्चों के आसन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को शारीरिक विकारों से बचाया जा सके। एक अच्छा आसन ही मनुष्य को एक अच्छी शारीरिक संरचना या बनावट और विभिन्न स्थितियों में संतुलित रख सकता है। इसलिए शारीरिक संतुलन विभिन्न क्रियाओं; जैसे खड़े होना, बैठना, चलना, लेटना, पढ़ना आदि को करते समय उचित होना चाहिए।
प्रश्न 2.
अच्छे आसन (मुद्रा) की महत्ता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
अथवा
अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छे आसन के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
शरीर की किसी एक स्थिति को मुद्रा नहीं कहा जाता बल्कि हम अपने शरीर को कई अलग-अलग ढंगों से स्थिर करते रहते हैं । शरीर को स्थिर रखने की स्थितियों को मुद्रा या आसन कहा जाता है। शरीर को बिना तकलीफ के उठाना, बैठाना, घुमाना आदि मुद्रा में ही आते हैं। शरीर की प्रत्येक प्रकार की स्थिति मुद्रा ही कहलाएगी। परंतु गलत और ठीक मुद्रा में बहुत अंतर होता है।
ठीक मुद्रा देखने में सुंदर व आकर्षक लगती है। इससे शरीर की माँसपेशियों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। ठीक मुद्रा वाला व्यक्ति काम करने, चलने-फिरने में चुस्त और फुर्तीला होता है। भद्दी मुद्रा व्यक्ति के शरीर के लिए अनावश्यक बोझ बन जाती है। इसलिए हमेशा शरीर की स्थिति प्रत्येक प्रकार का आसन (Posture) प्राप्त करते समय ठीक रखनी चाहिए।शरीर को अच्छी स्थिति में रखने से शरीर को हिलाना-डुलाना आसान हो जाता है और शरीर के दूसरे भागों पर भी भार नहीं पड़ता।
अच्छी मुद्रा मन को प्रसन्नता एवं खुशी प्रदान करती है। अच्छी मुद्रा वाले व्यक्ति की कार्य करने में शक्ति कम लगती है अर्थात् उसे कोई भी कार्य करने में कठिनाई नहीं होती। अच्छी मुद्रा हड्डियों और माँसपेशियों को संतुलित रखती है। अच्छी मुद्रा वाले व्यक्ति को बीमारियाँ कम लगती हैं । उचित आसन से व्यक्ति की शारीरिक आकृति आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देती है अर्थात् उसका शारीरिक ढाँचा बहुत आकर्षित दिखता है। इससे स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न 3.
आसन संबंधी विकृतियों या कुरूपताओं के कोई चार कारण बताएँ।
उत्तर:
आसन संबंधी विकृतियों या कुरूपताओं के कोई चार कारण निम्नलिखित हैं
1. बैठते, उठते, लेटते समय, खड़े होते समय तथा कार्य करते समय गलत आसन शरीर में कुरूपताएँ पैदा करते हैं। उदाहरणस्वरूप पढ़ते समय हम एक तरफ झुककर अथवा कुर्सी पर बैठकर, मेज पर झुककर पढ़ते हैं, फिर यह आदत बन जाती है, जिससे आसन में विकृति आ जाती है।
2. अधिक दबाव के कारण भी शरीर में विकृति आ जाती है। विशेषतौर पर बाल्यावस्था में माँसपेशियों तथा हड्डियों में अधिक दबाव हानिकारक होता है।
3. अधिक भारी शरीर हड्डियों, माँसपेशियों तथा लिगामेंट्स पर अधिक भार डालता है जिसके कारण आगे की ओर कूब (Lordosis), बाहर की तरफ मुड़ी हुई टाँगें (Bow Legs) तथा चपटे पैर (Flat Feet) जैसी कुरूपताएँ आ जाती हैं। अधिक भार से घुटनों के जोड़ों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
4. आसन में कुरूपताएँ आने का सबसे बड़ा कारण व्यायाम की कमी है, क्योंकि व्यायाम हमारी माँसपेशियों में शक्ति तथा नीरोगता लाते हैं। जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम नहीं करते, उनकी माँसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें कई बार स्थायी तौर पर कुरूपताएँ आ जाती हैं। व्यायाम बच्चे के आसन को सुंदरता प्रदान करते हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व में
वृद्धि होती है।
प्रश्न 4.
घुटनों के आपस में टकराने की विकृति को ठीक करने के उपाय बताएँ।
उत्तर:
घुटनों के आपस में टकराने की विकृति को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- इस विकृति को दूर करने के लिए टाँगों की ऐसी कसरतें करवानी चाहिएँ, जिनसे घुटनों को बाहर निकाला जा सके।
- इस विकृति को दूर करने के लिए साइकिल चलाई जानी चाहिए।
- इस विकृति को दूर करने में तैराकी और घुड़सवारी लाभदायक होती है।
- नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन करना चाहिए।
- कैल्शियम व फॉस्फोरस तथा विटामिन ‘डी’ युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए।
![]()
प्रश्न 5.
झुकी हुई या धनुषाकार टाँगों के क्या कारण हैं? इसके ठीक करने के उपाय बताएँ।
उत्तर:
झुकी हुई टाँगें एक आसन संबंधी कुरूपता है। अनुमानतः यह घुटनों के मुड़ने के बिल्कुल विपरीत है। जब व्यक्ति दोनों पाँव मिलाकर खड़ा हो और घुटनों में कोई स्पर्श न हो तो इसको झुकी हुई टाँगों की कुरूपता कहते हैं।
- कारण (Causes): झुकी हुई टाँगों के कारण निम्नलिखित होते हैं
- भोजन में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की कमी के परिणामस्वरूप हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं।
- हड्डियों पर अत्यधिक बोझ डालने वाले कार्य करने से।
- रिकेट्स रोग।
- लंबे समय तक खड़ा रहना।
- चलने तथा दौड़ने का अनुचित तरीका आदि।
- ठीक करने के उपाय (Remedial Measures): झुकी हुई टाँगों को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- कैल्शियम तथा फॉस्फोरस-युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए।
- सूर्य का प्रकाश तथा मछली के तेल को विटामिन ‘डी’ की पूर्ति हेतु लेना चाहिए।
- पाँवों की आंतरिक साइड पर दबाव डालकर चलने से झुकी हुई टाँगों की कुरूपता से बचा जा सकता है।
- वसा-युक्त भोजन को अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए।
प्रश्न 6.
रीढ़ की हड्डी के एक ओर झुके होने के क्या कारण हैं?
उत्तर:
रीढ़ की हड्डी के एक ओर झुके होने के कारण निम्नलिखित हैं
- हड्डियों के जोड़ों से संबंधित बीमारी होना।
- भोजन में आवश्यक तत्त्वों की कमी होना।
- अनुचित आसन धारण करना।
- रिकेट्स व पोलियो रोग होना।
- माँसपेशियों का कमजोर होना।
प्रश्न 7.
हमें उचित आसन की आवश्यकता क्यों होती है?
अथवा
अच्छे आसन की आवश्यकता पर संक्षेप में प्रकाश डालें।
उत्तर:
हमें उचित या अच्छे आसन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है
- शरीर को विकृतियों से बचाने हेतु।
- हड्डियों एवं माँसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु।
- शरीर में रक्त प्रवाह की गति सुचारू रूप से चलाने हेतु।
- व्यक्तित्व को आकर्षक व प्रभावशाली बनाने हेतु।
- शरीर में स्फूर्ति एवं उत्साह बनाए रखने हेतु।
- आत्म-विश्वास की भावना का विकास करने हेतु आदि।
प्रश्न 8.
चपटे पैरों के दोषों को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है?
अथवा
चपटे पैरों की विकृति को ठीक करने के मुख्य उपाय बताएँ।
उत्तर:
चपटे पैरों की विकृति को ठीक करने के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं
- पैरों में फिट आने वाले जूते पहनने चाहिएँ।
- चलते समय पैरों की बाहरी तरफ अधिक बल डालना चाहिए।
- एक अवस्था में लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना चाहिए।
- पंजों के बल दौड़ना व साइकिल चलानी चाहिए।
- भारी तथा असुविधाजनक जूते नहीं पहनने चाहिएँ।
- पैरों को इकट्ठा करके पंजों के बल बैठना चाहिए।
- पंजों पर वजन उठाकर व्यायाम करना चाहिए।
- इस विकृति को ठीक करने में घुड़दौड़ काफी लाभदायक है।
प्रश्न 9.
अनुचित आसन की प्रमुख हानियाँ संक्षेप में बताएँ।
उत्तर:
अनुचित आसन की हानियाँ निम्नलिखित हैं
- हड्डियों तथा माँसपेशियों में तालमेल नहीं हो पाता।
- थकान जल्दी हो जाती है।
- उठने, बैठने तथा चलने-फिरने में कठिनाई होती है।
- शारीरिक अंगों की शक्ति कम हो जाती है।
- जोड़ों में सहनशक्ति की कमी आ जाती है।
प्रश्न 10.
हम अपना आसन कैसे ठीक रख सकते हैं?
अथवा
आसनं ठीक रखने के महत्त्वपूर्ण उपायों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
आसन ठीक रखने के महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं
- बच्चों को ठीक आसन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। स्कूल में अध्यापकों और घर में माता-पिता का कर्तव्य है कि बच्चों के खराब आसन को ठीक करने के लिए योग्य प्रयास करें।
- भोजन की कमी के कारण आई कमजोरी को ठीक करना चाहिए।
- बच्चों को न तो तंग कपड़े पहनाने चाहिएँ और न ही तंग जूते।
- हमें गलत ढंग से न तो चलना चाहिए और न ही पढ़ना व बैठना चाहिए।
- पौष्टिक व संतुलित भोजन खाना चाहिए।
- बच्चों के स्कूल बैग का भार हल्का होना चाहिए।
- आवश्यकतानुसार डॉक्टरी परीक्षण करवाते रहना चाहिए ताकि आसन-त्रुटि को समय पर ठीक किया जा सके।
- घरों, स्कूलों और कॉलेजों में ठीक मुद्रा की जानकारी देने वाले चित्र लगे होने चाहिएँ।
प्रश्न 11.
बैठने का उचित आसन कैसा होना चाहिए?
अथवा
बैठने की मुद्रा (Posture) पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
उत्तर:
बहुत-से ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए हमें अधिक देर तक बैठना पड़ता है। अधिक देर बैठने से धड़ की माँसपेशियाँ थक जाती हैं और धड़ में कई दोष आ जाते हैं । बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती आमतौर पर खुली, कंधे समतल, पेट स्वाभाविक तौर पर अंदर की ओर, सिर और धड़ सीधी स्थिति में होने चाहिएँ। बैठने वाला स्थान हमेशा खुला, समतल तथा साफ-सुथरा होना चाहिए। देखा जाता है कि कई व्यक्ति सही ढंग से बैठकर नहीं पढ़ते।
पढ़ते समय मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिससे आँखों व शरीर पर कम-से-कम दबाव पड़े। लिखने के लिए मेज या डैस्क का झुकाव आगे की ओर होना चाहिए। हमें कभी भी सिर झुकाकर न तो पढ़ना चाहिए और न ही लिखना चाहिए। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गलत ढंग से बैठने से शरीर में कई विकार पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें उचित आसन में ही बैठना चाहिए।
प्रश्न 12.
चलते समय शरीर का आसन किस तरह होना चाहिए?
अथवा
चलने के उचित आसन के बारे में लिखिए।
उत्तर:
चलने का आसन व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है । चलते समय पैर समानांतर रखने चाहिएँ। सिर को सीधा रखना चाहिए तथा कंधे पीछे की तरफ होने चाहिएँ। छाती तनी हुई तथा बाजुएँ बिना किसी तनाव के झूलनी चाहिएँ । चलते समय पैर आपस में टकराने नहीं चाहिएँ तथा शरीर की माँसपेशियाँ साधारण स्थिति में होनी चाहिएँ । चलते समय ठीक आसन ही अपनाया जाना चाहिए ताकि शरीर में कम-से-कम थकावट हो सके । गलत आसन में चलने से शारीरिक ढाँचा ठीक नहीं रहता, क्योंकि इससे न सिर्फ टाँगें तथा माँसपेशियाँ थकती हैं, अपितु टाँगों तथा पैरों में दर्द भी होता रहता है। इसलिए हमें चलते समय अपने आसन को उचित रखना चाहिए।
प्रश्न 13.
रीढ़ की हड्डी का पीछे की तरफ कूब (Kyphosis) के प्रमुख कारण बताएँ।
उत्तर:
रीढ़ की हड्डी का पीछे की तरफ कूब होने के कारण निम्नलिखित हैं
- आगे की ओर झुककर पढ़ने तथा काम करने से।
- व्यायाम की कमी के कारण।
- लंबा कद होने के कारण।
- बीमारी अथवा दुर्घटना होने के कारण।
- बैठने के लिए अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करने के कारण।
- शारीरिक कमजोरी व विकार के कारण।
- लंबे समय तक अनुचित मुद्रा में बैठने के कारण आदि।
प्रश्न 14.
रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर कूब (Lordosis) होने के कारण बताएँ।
उत्तर:
रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ कूब होने के कारण निम्नलिखित हैं
- छाती को आगे की तरफ निकालकर चलने की आदत।
- व्यायाम की कमी के कारण।
- छाती तथा गर्दन की कमजोर माँसपेशियों के कारण।
- संतुलित भोजन की कमी के कारण।
- गलत आसन धारण करने के कारण।
![]()
प्रश्न 15.
रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ कूब को ठीक करने के उपाय बताएँ।
उत्तर:
रीढ़ की हड्डी का आगे की तरफ कूब को ठीक करने के उपाय निम्नलिखित हैं
- पीठ के बल लेटने वाले व्यायाम करना।
- खड़े होकर धड़ को अगली तरफ झुकाना।
- गर्दन तथा कंधों को आगे की ओर झुकाकर लंबे-लंबे साँस लेना।
- पैरों को जोड़कर हाथों से पैरों को छूना।
- हलासन तथा पद्मासन इस कुरूपता के लिए लाभदायक हैं।
अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न (Very ShortAnswer Type Questions)
प्रश्न 1.
उचित आसन से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
आसन या मुद्रा शरीर की स्थिति को कहते हैं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लेटना आदि। अच्छे आसन से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर का ठीक एवं उचित संतुलन में होना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते हुए उचित या अच्छा होना चाहिए। वास्तव में एक खड़े हुए व्यक्ति का उचित आसन उस अवस्था में होगा, जब उसके शरीर का भार उसके दोनों पैरों पर एक-समान होगा।
प्रश्न 2.
उचित आसन के कोई दो फायदे बताएँ।
उत्तर:
- उचित आसन से व्यक्ति की शारीरिक आकृति आकर्षक एवं सुंदर दिखाई देती है अर्थात् उसका शारीरिक ढाँचा आकर्षित दिखता है,
- इससे शरीर के सभी संस्थान सुचारू रूप से कार्य करते हैं।
प्रश्न 3.
लेटते समय कौन-कौन-सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर:
- लेटते समय शरीर विश्राम की स्थिति में होना चाहिए,
- लेटते समय कठोर गद्दे का प्रयोग करना चाहिए,
- कभी भी लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए।
प्रश्न 4.
आगे की ओर कूब को ठीक करने की शारीरिक क्रियाएँ बताएँ।
उत्तर:
1. छाती के बल लेटकर अपने दोनों हाथ उदर पर रखें। इसके बाद कूल्हों एवं कंधों को नीचे रखें। फिर पीठ के निचले भाग को उठाने का प्रयास करें। इस प्रकार से यह क्रिया 5-6 बार दोहराएँ।
2. फर्श पर अधोमुख अवस्था में लेटकर अपने कंधों की चौड़ाई के अनुसार अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ फर्श पर रखें। श्रोणी (Pelvis) को फर्श पर रखते हुए धड़ को ऊपर की ओर ले जाएँ। इस अवस्था में कुछ देर तक रहने के बाद पहले वाली अवस्था में आ जाएँ। इस प्रकार से यह प्रक्रिया कई बार दोहराएँ।
प्रश्न 5.
चपटे पैरों की विकृति के कोई तीन लक्षण बताएँ।
उत्तर:
- पैरों की कमजोर माँसपेशियाँ,
- अधिक वजन उठाना,
- लंबे समय तक जूतों का प्रयोग किए बिना खड़े रहना।
प्रश्न 6.
घुटनों के आपस में टकराने के क्या कारण हैं?
उत्तर:
छोटे बच्चों के भोजन में कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन ‘डी’ की कमी के कारण उनकी हड्डियाँ कमजोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं। इस कारण उनके घुटने टकराने लग जाते हैं। इस स्थिति में उन बच्चों से सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं हुआ जाता। उनके पाँव टकराने लगते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अच्छी तरह भागना तथा चलना मुश्किल होता है।
प्रश्न 7.
रीढ़ की हड्डी संबंधी विकृतियाँ बताएँ।
उत्तर:
- पीछे की तरफ कूब होना या काइफोसिस,
- आगे की तरफ कूब होना या लॉर्डोसिस,
- स्कोलिओसिस।
प्रश्न 8.
अनुचित आसन से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
शरीर की स्थिति ठीक अवस्था में न होना अनुचित आसन कहलाता है; जैसे चलते, बैठते, पढ़ते, लिखते व खड़े होते समय शरीर का उचित अवस्था या स्थिति में न रहना अनुचित आसन कहलाता है।
प्रश्न 9.
चपटे पैरों की विकृति को सुधारने हेतु लाभदायक व्यायाम बताएँ।
उत्तर:
- नियमित रूप से रस्सी कूदना,
- सीधा खड़े होकर एड़ियों को ऊपर-नीचे करना,
- पंजों पर कूदना।
प्रश्न 10.
घुटनों के टकराने की विकृति को सुधारने हेतु लाभदायक व्यायाम बताएँ।।
उत्तर:
- नियमित रूप से आसन करना, मुख्य रूप से पद्मासन व गोमुखासन अधिक लाभदायक हैं,
- घुड़सवारी करना,
- कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधा खड़े होना।
प्रश्न 11.
अनुचित आसन के कोई दो कारण लिखें।
उत्तर:
- पौष्टिक व संतुलित आहार का अभाव,
- आसन संबंधी बुरी आदतें।
![]()
प्रश्न 12.
पढ़ते समय कैसा आसन रखना चाहिए?
उत्तर:
पढ़ते समय व्यक्ति का आसन इस प्रकार का होना चाहिए, जिससे उसके शरीर तथा आँखों पर कम-से-कम दबाव पड़े। पढ़ते समय किताब से आँखों की दूरी उचित होनी चाहिए। किताब इस प्रकार पकड़नी चाहिए जिससे उस पर रोशनी ठीक पड़ सके।आँखों के बिल्कुल समीप तथा बहुत दूर रखी हुई किताब कभी नहीं पढ़नी चाहिए।
प्रश्न 13.
बैठते समय कौन-कौन-सी कमियाँ शरीर के ढाँचे को खराब करती हैं?
उत्तर:
- ढीले शरीर से बैठना,
- कुर्सी पर बैठते समय बच्चे के पैर फर्श पर न लगना,
- कुर्सी बहुत नीचे होना,
- एक ओर साइड लेकर बैठना,
- बैठते समय टाँगों की सही चौंकड़ी न मारना।
प्रश्न 14.
क्या ठीक चाल शरीर को आकर्षक बनाती है?
उत्तर:
हाँ, ठीक चाल शरीर को आकर्षक बनाती है। चलना एक कला है। चलते समय पंजे और एड़ी पर बराबर भार पड़ना चाहिए। अच्छी चाल शरीर को प्रभावशाली और आकर्षक बनाती है।
प्रश्न 15.
झुकी हुई टाँगों की विकृति के कोई तीन कारण बताएँ।
उत्तर:
- भोजन में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की कमी के परिणामस्वरूप हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं,
- रिकेट्स रोग,
- चलने तथा दौड़ने का अनुचित तरीका।
प्रश्न 16.
हमें किस प्रकार खड़े होना चाहिए? खड़े होने का उचित आसन क्या है?
उत्तर:
ठीक ढंग से खड़े होने की आदत डालने के लिए हमेशा दोनों पैरों पर बराबर भार डालकर खड़े होना चाहिए। खड़े होते समय पेट सीधा, छाती फैली हुई और धड़ सीधी होनी चाहिए।
प्रश्न 17.
गोल कंधों को ठीक करने के कोई दो सुधारात्मक व्यायाम बताएँ।
उत्तर:
- नियमित रूप से हॉरिजौटल बार पर कुछ देर तक लटके रहना,
- चक्रासन एवं धनुरासन करना।
प्रश्न 18.
आसन संबंधी सामान्य विकृतियाँ बताएँ।
उत्तर:
- चपटे पैर (Flat Foot),
- घुटनों का आपस में टकराना (Knock Knee),
- टाँगों का बाहरी ओर मुड़ा होना (Bow Legs),
- लॉर्डोसिस (Lordosis),
- काइफोसिस (Kyphosis),
- स्कोलिओसिस (Scoliosis)।
प्रश्न 19.
शरीर के आसन खराब होने के सामान्य कारण कौन-कौन-से हो सकते हैं?
उत्तर:
- संतुलित भोजन की कमी,
- व्यायाम न करना,
- पढ़ते समय बैठने के लिए सही कुर्सी एवं मेज का न होना,
- छोटे बच्चों द्वारा भारी बस्ता उठाना।
प्रश्न 20.
गोल कंधे होने के क्या कारण हैं?
उत्तर:
- आनुवांशिकता संबंधी दोष,
- उचित आसन धारण न करना अर्थात् झुकी हुई अवस्था में बैठना, खड़े होना आदि,
- व्यायाम न करना,
- अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करना।
HBSE 11th Class Physical Education आसन Important Questions and Answers
वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)
भाग-I : एक वाक्य में उत्तर देंप्रश्न
1. आसन क्या है?
उत्तर:
शरीर द्वारा कोई टिकाऊ स्थिति ग्रहण करने को आसन कहते हैं।
प्रश्न 2.
उचित आसन देखने में कैसा लगता है?
उत्तर;
उचित आसन देखने में आकर्षक और प्रभावशाली लगता है।
प्रश्न 3.
उचित आसन व्यक्ति को कैसे रखता है?
उत्तर:
उचित आसन व्यक्ति को चुस्त, तेज और बीमारियों से बचाकर रखता है।
प्रश्न 4.
“एक संतुलित आसन वह है जिसमें शरीर संतुलित हो, जिससे कम-से-कम थकावट उत्पन्न हो।” यह कथन किसका है?
उत्तर:
एवेरी का।
प्रश्न 5.
पीछे की तरफ कूब वाली कुरूपता में रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का रूप धारण कर लेती है?
उत्तर:
पीछे की तरफ कूब वाली कुरूपता में रीढ़ की हड्डी कमान के आकार का रूप धारण कर लेती है।
प्रश्न 6.
आगे की ओर कूब वाली कुरूपता शरीर के किस अंग से संबंधित है?
उत्तर:
आगे की ओर कूब वाली कुरूपता रीढ़ की हड्डी से संबंधित है।
प्रश्न 7.
वह कौन-सी कुरूपता है जिसमें छाती अगली तरफ तथा गर्दन पिछली तरफ झुक जाती है?
उत्तर:
आगे की ओर कूब का निकलना या लॉर्डोसिस।
प्रश्न 8.
छाती को अगली तरफ सीधा करके चलना-फिरना किस कुरूपता के लिए लाभदायक है?
उत्तर;
छाती को अगली तरफ सीधा करके चलना-फिरना पीछे की तरफ निकले कूब के लिए लाभदायक है।
![]()
प्रश्न 9.
चपटे पैरों की विकृति या कुरूपता का कोई एक लक्षण बताएँ।
उत्तर:
पैरों में भौरियाँ निकलना।
प्रश्न 10.
पैरों की माँसपेशियाँ कमजोर होने के कारण पैरों के जोड़ कैसे हो जाते हैं?
उत्तर:
पैरों की माँसपेशियाँ कमजोर होने के कारण पैरों के जोड़ सीधे हो जाते हैं।
प्रश्न 11.
आसन संबंधी कुरूपताओं का कोई एक कारण बताएँ। अथवा भद्दी मुद्रा का कोई एक कारण लिखें।
उत्तर:
हड्डियाँ व माँसपेशियाँ कमजोर होना।
प्रश्न 12.
बच्चे के बैठने के लिए कुर्सी किस प्रकार की होनी चाहिए?
उत्तर:
बच्चे के बैठने के लिए कुर्सी बच्चे के कद के अनुसार होनी चाहिए।
प्रश्न 13.
बैठते समय किस प्रकार नहीं बैठना चाहिए?
उत्तर:
बैठते समय शरीर ढीला छोड़कर दाईं और बाईं ओर भार डालकर नहीं बैठना चाहिए।
प्रश्न 14.
हमें कुर्सी पर किस प्रकार बैठना चाहिए?
उत्तर:
हमें कुर्सी पर आगे की ओर झुककर नहीं, बल्कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए।
प्रश्न 15.
लेटकर पढ़ना हानिकारक क्यों है?
उत्तर:
लेटकर पढ़ने से आँखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
प्रश्न 16.
शारीरिक आसन को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए?
उत्तर:
शारीरिक आसन को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए।
प्रश्न 17.
अच्छे आसन का कोई एक सामान्य नियम बताएँ।
उत्तर:
शरीर के विभिन्न अंगों के प्रभावशाली कार्य अर्थात् क्रियाओं का प्रभावशाली होना।
प्रश्न 18.
किसकी कमी के कारण बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं?
उत्तर:
संतुलित व पौष्टिक भोजन की कमी के कारण बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं।
प्रश्न 19.
धनुषाकार टाँगों के विपरीत कौन-सी आसन संबंधी विकृति होती है?
उत्तर:
घुटनों का आपस में टकराना (Knock Knee)।
प्रश्न 20.
अच्छे आसन वाला व्यक्ति अपने काम कैसे कर सकता है?
उत्तर:
अच्छे आसन वाला व्यक्ति अपने काम चुस्ती और फूर्ति के साथ कर सकता है।
प्रश्न 21.
ठीक आसन का ज्ञान देने के लिए स्कूलों में कौन-सी चीज का प्रबंध करना चाहिए?
उत्तर:
ठीक आसन का ज्ञान देने के लिए स्कूलों में ठीक आसन के चित्र लगाने चाहिएँ।
प्रश्न 22.
आगे की ओर कूब में सुधार हेतु कोई दो लाभदायक आसन बताएँ।
उत्तर:
हलासन, पद्मासन।
प्रश्न 23.
विटामिन ‘डी’ की कमी से कौन-सी विकृति हो सकती है?
उत्तर:
विटामिन ‘डी’ की कमी से रीढ़ की हड्डी मुड़ सकती है।
![]()
प्रश्न 24.
आगे या पीछे की ओर कूबड़ काली विकृति किस अंग से संबंधित है?
उत्तर:
आगे या पीछे की ओर कूबड़ वाली विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित है।
प्रश्न 25.
साइकिल चलाना, तैराकी और घुड़सवारी किस प्रकार की विकृति को ठीक करने में लाभदायक हैं?
उत्तर:
साइकिल चलाना, तैराकी और घुड़सवारी घुटने के आपस में टकराने की विकृति को ठीक करने में लाभदायक हैं।
प्रश्न 26.
अधोमुख अवस्था कौन-सी होती है?
उत्तर:
यह शरीर की ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की छाती नीचे और पीठ ऊपर की ओर होती है।
भाग-II : सही विकल्प का चयन करें
1. आसन का अर्थ है
(A) लेटना
(B) सोना
(C) व्यक्ति के शरीर की स्थिति
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) व्यक्ति के शरीर की स्थिति
2. मनुष्य के अच्छे आसन का पता चलता है
(A) खड़े होने से
(B) चलने से
(C) बैठने से
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
3. निम्नलिखित में से मुद्रा या आसन संबंधी सामान्य समस्या है
(A) स्कोलिओंसिस (Scoliosis)
(B) लॉर्डोसिस (Lordosis)
(C) काइफोसिस (Kyphosis)
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
4. अनुचित आसन के कारण हैं
(A) शारीरिक बीमारियाँ
(B) संतुलित व पौष्टिक आहार की कमी
(C) गलत आदतें
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
5. शरीर को सीधा खड़ा रखने में आधार प्रदान करने वाली माँसपेशियाँ होती हैं
(A) हाथों की माँसपेशियाँ
(B) पैरों की माँसपेशियाँ
(C) छाती की माँसपेशियाँ
(D) कूल्हे की माँसपेशियाँ
उत्तर:
(B) पाँवों की माँसपेशियाँ
6. अच्छे आसन के सामान्य नियम हैं
(A) प्रभावशाली क्रियाओं का होना
(B) शरीर के विभिन्न अंगों के प्रभावशाली कार्य
(C) माँसपेशी व अस्थिपिंजर संस्थानों पर असाधारण
(D) उपर्युक्त सभी दबाव का न होना
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
![]()
7. “खड़े रहने का अच्छा आसन तभी कहा जा सकता है यदि खड़े रहते समय कम-से-कम शक्ति खर्च की जाए।” यह कथन है
(A) करूगर का
(B) डॉ० थॉमस वुड का
(C) रॉस का
(D) जे० बी० नैश का
उत्तर:
(A) करूगर का
8. शरीर का संपूर्ण भार किन पर पड़ता है?
(A) माँसपेशियों पर
(B) हड्डियों पर
(C) हाथों पर
(D) नाड़ियों पर
उत्तर:
(B) हड्डियों पर
9. पढ़ते समय आँखों से किताब की दूरी कम-से-कम होनी चाहिए
(A) 30 सें०मी०
(B) 25 सें०मी०
(C) 15 सें०मी०
(D) 20 सें०मी०
उत्तर:
(A) 30 सें.मी०
10. मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण कहा जाने वाला आसन है
(A) खड़े रहने का आसन
(B) बैठने का आसन
(C) पढ़ते समय का आसन
(D) चलते समय का आसन
उत्तर:
(D) चलते समय का आसन
11. चलते समय पैर होने चाहिएँ
(A) असमानांतर
(B) 60° कोण पर
(C) समानांतर
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) समानांतर
12. लेटते समय पैर रखने चाहिएँ
(A) असमानांतर
(B) मुड़े हुए
(C) जुड़े हुए
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(C) जुड़े हुए
13. अच्छे आसन का लाभ है
(A) हड्डियों और माँसपेशियों में तालमेल
(B) आत्म-विश्वास में वृद्धि
(C) शारीरिक योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
14. अनुचित आसन के संबंध में असत्य है
(A) व्यक्तित्व में कमी
(B) कंधे ढल जाना
(C) शरीर का सीधा तथा एकरूपता में होना
(D) आत्म-विश्वास की कमी
उत्तर:
(C) शरीर का सीधा तथा एकरूपता में होना
15. ठीक आसन व्यक्ति को कैसे रखता है?
(A) चुस्त
(B) तेज
(C) नीरोग
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
16. चपटे पैरों की कुरूपता का लक्षण नहीं है
(A) पैरों का सुन्न रहना
(B) पैरों में भौरियों का निकलना
(C) शरीर में स्फूर्ति बढ़ना
(D) पैरों में अधिक पसीने का आना
उत्तर:
(C) शरीर में स्फूर्ति बढ़ना
17. उचित आसन हमारे लिए किस कारण महत्त्वपूर्ण है?
(A) इससे शरीर में स्फूर्ति एवं उमंग बढ़ती है
(B) शारीरिक संस्थान सुचारू रूप से कार्य करते हैं
(C) शारीरिक अंगों का उचित विकास होता है
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
18. आगे की तरफ कूब को ठीक करने का उपाय है
(A) पीठ के बल लेटने वाला व्यायाम करना
(B) हलासन एवं पद्मासन करना
(C) खड़े होकर धड़ को अगली तरफ झुकाना
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
19. टाँगें झुकी हुई या धनुषाकार किस बीमारी के कारण होती हैं?
(A) कैंसर
(B) रिकेट्स
(C) टी०बी०
(D) मलेरिया
उत्तर:
(B) रिकेट्स
![]()
20. घुटनों के आपस में टकराने से संबंधित शारीरिक क्रिया है
(A) साइकिल चलाना
(B) घुड़सवारी करना
(C) पद्मासन करना
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
21. आसन संबंधी कुरूपताओं का कारण है
(A) शरीर का अधिक भारी होना
(B) कमजोर हड्डियाँ तथा माँसपेशियाँ
(C) गलत आसन तथा बुरी आदतें
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
22. रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है
(A) ठीक प्रकार से न बैठने पर
(B) गलत ढंग से चलने से
(C) ठीक प्रकार से न खड़े होने पर
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
23. पीछे की तरफ कूब वाली कुरूपता का मुख्य कारण है
(A) आगे की ओर झुककर पढ़ना
(B) व्यायाम की कमी
(C) संतुलित आहार की कमी
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
24. पीछे की तरफ कूब वाली कुरूपता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा व्यायाम/आसन काफी लाभदायक है?
(A) भुजंगासन
(B) शलभासन
(C) सर्वांगासन व चक्रासन
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
भाग-III : निम्नलिखित कथनों के उत्तर सही या गलत अथवा हाँ या नहीं में दें
1. उचित/संतुलित आसन से शारीरिक थकान बढ़ती है। (हाँ/नहीं)
उत्तर:
नहीं,
2. उचित आसन से शारीरिक पुष्टि कम होती है। (हाँ/नहीं)
उत्तर:
नहीं,
3. उचित आसन हेतु नियमित रूप से व्यायाम करने चाहिएँ। (सही/गलत)
उत्तर:
सही,
4. उचित आसन से शरीर में स्फूर्ति एवं उमंग बढ़ती है। (हाँ/नहीं)
उत्तर:
हाँ,
5. आसन (मुद्रा) से अभिप्राय मन की स्थिति से है। (सही/गलत)
उत्तर:
गलत
6. संतुलित आसन से विभिन्न प्रकार के कौशलों की संपूर्णता में सुधार होता है। (सही/गलत)
उत्तर:
सही,
7. हमें कभी भी सिर को झुकाकर नहीं पढ़ना चाहिए। (सही/गलत)
उत्तर:
सही,
8. चलने का आसन व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। (सही/गलत)
उत्तर:
सही,
9. तैरने से रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन में लाभ होता है। (हाँ/नहीं)
उत्तर:
हाँ,
10. रीढ़ की हड्डी का शरीर के दाईं या बाईं ओर झुकना या मुड़ना स्कोलिओसिस कहलाता है। (सही/गलत)
उत्तर:
सही,
![]()
11. चपटे पैरों की विकृति को ठीक करने के लिए साइक्लिंग और घुड़दौड़ काफी लाभदायक हैं। (हाँ/नहीं)
उत्तर:
हाँ,
12. आसन में विकृतियों के आने का मुख्य कारण व्यायाम करना है। (सही/गलत)
उत्तर:
गलत
13. अधिक देर तक बैठे रहने से धड़ की माँसपेशियाँ मजबूत होती हैं। (सही/गलत)
उत्तर:
गलत
14. जल्दी सोना अच्छी आदत है। (सही/गलत)
उत्तर:
सही,
भाग-IV : रिक्त स्थानों की पूर्ति करें
1. व्यक्ति का शारीरिक आभास (Appearance) उसके ……………. पर निर्भर करता है।
उत्तर:
आसन,
2. घुटनों के आपस में टकराने को सुधारने के लिए नियमित रूप से पद्मासन और ………………. करना चाहिए।
उत्तर:
गोमुखासन,
3. गोल कंधों की विकृति को सुधारने के लिए …………….. बार पर कुछ देर तक लटकना चाहिए।
उत्तर:
हॉरिजौंटल
4. उचित आसन वाला व्यक्ति किसी कार्य को करने में …………….. ऊर्जा व्यय करता है।
उत्तर:
कम,
5. आसन से अभिप्राय …………….. की स्थिति से है।
उत्तर:
शरीर,
6. आसन संबंधी विकृतियों में सुधार हेतु नियमित रूप से ………… करने चाहिएँ।
उत्तर:
व्यायाम,
7. अनुचित आसन धारण करने से …………… शारीरिक विकारों को बढ़ावा मिलता है।
उत्तर:
अनुचित,
8. उचित आसन से शारीरिक पुष्टि …………….. है।
उत्तर:
बढ़ती,
9. उचित आसन से शरीर के ………….. दूर होते हैं।
उत्तर:
विकार,
10. ……………. आसन आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान को बढ़ावा देता है।
उत्तर:
उचित,
![]()
11. …………….. मुद्रा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है।
उत्तर:
भद्दी,
12. शरार का स्थात ठाक अवस्था में न होना …………….. आसन कहलाता है।
उत्तर:
अनुचित।
आसन Summary
आसन परिचय
मुद्रा या आसन (Posture) का मानवीय-जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। आसन से अभिप्राय शरीर की स्थिति से है अर्थात् मनुष्य किस प्रकार अपने शरीर की संभाल या देखरेख करता है। आसन की अवहेलना करना मानो कई प्रकार के शारीरिक दोषों या विकारों को निमंत्रित करना है। इसलिए बचपन से ही बच्चों के आसन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को शारीरिक विकारों से बचाया जा सके। एक अच्छा आसन ही मनुष्य को एक अच्छी शारीरिक संरचना या बनावट प्रदान कर सकता है और विभिन्न स्थितियों में संतुलित रख सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन या व्यक्तित्व में उचित आसन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन के प्रत्येक पहलू या पक्ष में इसकी अहम् भूमिका होती है।
उचित आसन से अभिप्राय व्यक्ति के शरीर का ठीक अथवा उचित संतुलन में होना है। वास्तव में, व्यक्ति के अच्छे आसन का उसके खड़े होने, चलने तथा बैठने से पता लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का संतुलन विभिन्न क्रियाओं; जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, लिखना, पढ़ना, लेटना आदि को करते समय उचित या अच्छा होना चाहिए। उचित आसन से न केवल व्यक्ति का शारीरिक ढाँचा व स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि उसमें आत्म-विश्वास की भावना भी विकसित होती है। उसका व्यक्तित्व भी आकर्षित होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित आसन बहुत आवश्यक है। उचित आसन हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से महत्त्वपूर्ण है
- इससे शरीर में स्फूर्ति एवं उमंग बढ़ती है।
- इससे शरीर के सभी अंगों का उचित विकास होता है, क्योंकि इससे शारीरिक विकार दूर होते हैं।
- इससे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है।
- इससे मन की तत्परता का पता चलता है अर्थात् यह मानसिक या बौद्धिक विकास में सहायक होता है।
- इससे शरीर के सभी संस्थान सुचारू रूप से कार्य करते हैं।
- यह व्यक्ति के सम्मान और नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक होता है।
- अच्छी मुद्रा या आसन से माँसपेशी, श्वसन, पाचन एवं नाड़ी आदि शारीरिक संस्थानों की क्षमता में सुधार होता है और आपसी तालमेल भी बढ़ता है।
- अच्छे आसन से विभिन्न प्रकार के कौशलों की संपूर्णता में सुधार होता है।
- अच्छे आसन से व्यक्तित्व सुंदर एवं आकर्षित दिखता है।
- अच्छे आसन से शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं में सुधार होता है और मन की तत्परता व शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है।
- अच्छे आसन से समाजीकरण की योग्यता का पता चलता है। यह व्यक्ति के समाज में उच्च-स्तर का द्योतक है।
HBSE 11th Class Physical Education Solutions Chapter 5 आसन Read More »