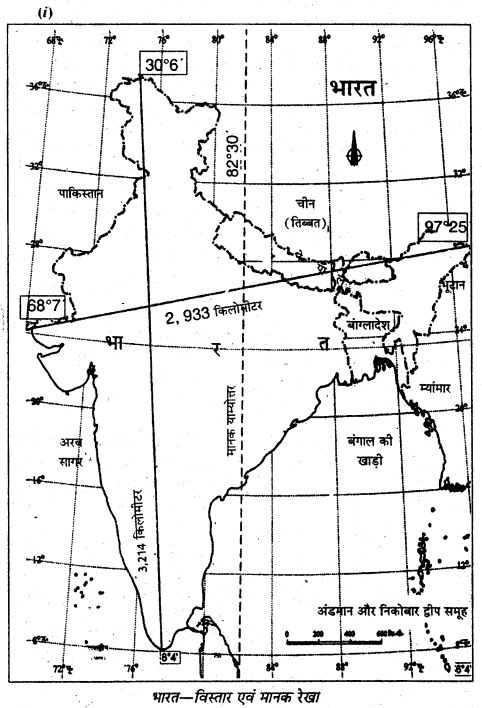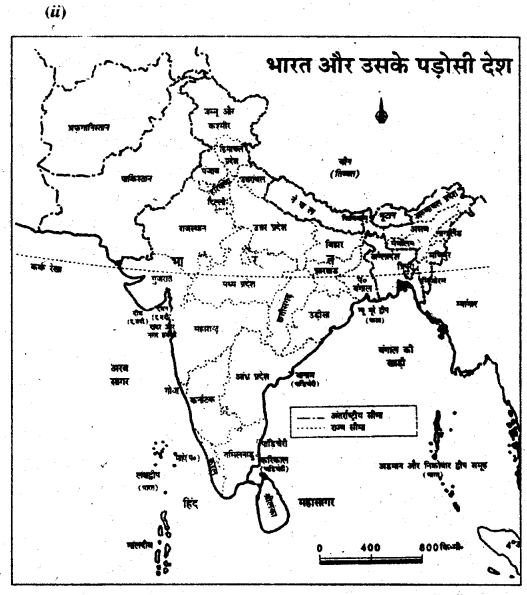HBSE 9th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 2 मेरे संग की औरतें
Haryana State Board HBSE 9th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 2 मेरे संग की औरतें Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 9th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 2 मेरे संग की औरतें
HBSE 9th Class Hindi मेरे संग की औरतें Textbook Questions and Answers
मेरे संग की औरतें के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 1.
लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं ?
उत्तर-
लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। विशेषकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में भी उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी से करना चाहती थी, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा से उनकी देशभक्ति का बोध होता है। इसके अतिरिक्त वह साहसी स्त्री थी। उन्होंने पर्दे में रहने के बावजूद किसी पराए पुरुष से मिलने का साहस किया था। इन तथ्यों से पता चलता है कि वह एक वीर स्त्री थी। उनके मन में स्वतंत्रता की आग सुलग रही थी। लेखिका उनके इन्हीं गुणों के कारण प्रभावित थी।
Mere Sang Ki Auraten Class 9 HBSE प्रश्न 2.
लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही ? [H.B.S.E. 2018, 2019]
उत्तर-
लेखिका की नानी की प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं रही। उसकी परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं कि वह खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं ले सकती थी। किंतु उसके मन में स्वतंत्रता-प्राप्ति की भावना सदा बनी रही। उसने कभी भी अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं की। उसके पति इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करके आए थे और अंग्रेज़ों के भक्त थे। फिर भी उसने अंग्रेज़ों की जीवन-शैली में कभी भाग नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा योगदान था कि उसने अपनी संतान को अंग्रेज़-भक्तों के चंगुल से मुक्त कर दिया था, ताकि उसकी संतान देश के लिए कुछ कर सके। इस प्रकार उनकी इस भावना से निश्चित रूप से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भागीदारी थी।
![]()
मेरे संग की औरतें’ पाठ 2 के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 3.
लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में
(क) लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएँ लिखिए। (ख) लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द-चित्र अंकित कीजिए।
उत्तर-
(क) लेखिका की माँ असाधारण व्यक्तित्व वाली महिला थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। वे मौलिक विचारों वाली स्त्री थीं। लेखिका ने लिखा है कि वे स्वयं अपने ढंग से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उनसे घर-गृहस्थी का कोई काम नहीं करवाया जाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि ठोस कामों के लिए उनसे राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की माँ को किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक भी था। उसके मान-सम्मान के दो बड़े कारण थे कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी की गोपनीय बात को दूसरों से नहीं कहती थी।
(ख) लेखिका की दादी एक विचित्र व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। वह लीक से हटकर काम करने वाली महिला थी। उसके घर में हर व्यक्ति को अपना अधिकार बनाए रखने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की दादी, ताई व पिता उसकी माँ के कर्त्तव्यों को पूरा करते थे। लेखिका की माँ बिस्तर पर लेटे-लेटे किताबें पढ़ती और संगीत सुनती। फिर भी उसे भरपूर सम्मान मिलता था। हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचार रखता था, किंतु फिर भी आपसी सद्व्यवहार का वातावरण बना रहता था। वहाँ किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं था। अतः किसी को भी हीन भावना अनुभव नहीं करनी पड़ती थी।
मेरे संग की औरतें प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 4.
आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों माँगी ?
उत्तर-
परदादी परंपरा की लीक पर चलने वाली स्त्री नहीं थी। उस युग में लड़की होने की मन्नत माँगना क्रांतिकारी विचार होने का संकेत करता है। उसकी दृष्टि में लड़की-लड़के में भेद नहीं था। उस युग में स्त्री-सुधार आंदोलन भी जोरों पर था। उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दादी पर अवश्य पड़ा होगा। उनकी मन्नत से यह पता चलता है कि उनकी दृष्टि में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। वह लड़कियों से प्रेम करती होगी इसलिए उसने लड़की होने की मन्नत माँगी होगी। परिवार में सब बहुओं को पहला लड़का ही हुआ था। इसलिए उसने पोते की बहू के लिए पहली लड़की होने की मन्नत माँगी होगी।
Mere Sang Ki Auraten HBSE 9th Class प्रश्न 5.
डराने-धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है-पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। .
उत्तर-
माँ जी जब एक रात रतजगे के शोर से बचने के लिए अलग कमरे में सो रही थीं, तब उनके कमरे में सेंध लगाकर कोई चोर घुस आया था। माँ जी आवाज़ सुनकर जाग गई और पूछा कौन है ? चोर द्वारा संक्षिप्त-सा उत्तर देने पर माँ जी ने उससे पानी लाने के लिए कहा। माँ जी ने कहा कि कपड़ा कसकर बाँधे रहना। चोर डर गया कि उसने कैसे जान लिया कि उसने कपड़ा बाँधा हुआ है। माँ जी ने चोर द्वारा बताने पर भी कि वह चोर है, पानी भरवाया। उसने लोटे से पानी पीकर शेष पानी चोर को पिला दिया और फिर कहा कि अब हम माँ-बेटा हुए। अब तू चोरी कर या खेती। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती का काम करना आरंभ कर दिया। इस घटना से सिद्ध होता है कि डराने-धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता से भी किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाया जा सकता है।
Kritika Chapter 2 Class 9 Answers HBSE प्रश्न 6.
‘शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
लेखिका मानती है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे-से कस्बे बागलकोट में थीं, तब वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, किंतु वे वहाँ इसलिए स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। किंतु लेखिका तो सब बच्चों के द्वारा शिक्षा पाने की पक्षपाती थी। उसके मन में किसी प्रकार का धर्म व जातिगत भेदभाव नहीं था। उसने अपने प्रयासों से ऐसा स्कूल आरंभ किया जिसमें बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ तीनों भाषाएँ पढ़ाई जाती थी। इसे कर्नाटक की सरकार से मान्यता भी दिला दी थी।
Class 9 Chapter 2 Kritika HBSE प्रश्न 7.
पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है ?
उत्तर–
प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि उन इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है, जिनमें निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं
(1) जो सदा सच बोलते हैं।
(2) जो किसी की गोपनीय बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते।
(3) जो अपने इरादों में दृढ़ रहते हों और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हों।
(4) जो दूसरों के साथ सहज व्यवहार करते हों।
(5) जिनमें हीन भावना न हो।
(6) जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हों।
मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर HBSE 9th Class प्रश्न 8.
‘सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है’-इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए।
उत्तर-
लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने जीवन-पथ पर चलने का पूर्ण साहस था। लेखिका ने अपनी हिम्मत और साहस से बिहार में रहते हुए नारी जागरण का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नारी-जागृति उत्पन्न करने के लिए उनमें एक अजीब धुन थी। इसी प्रकार उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल आरंभ किया था।
लेखिका की बहन रेणु भी जीवन में अकेले ही अनोखे काम कर दिखाने में आनंद अनुभव करने वाली युवती थी। उसे स्कूल से लौटते समय थोड़ी दूर के लिए गाड़ी में आना पसंद नहीं था। वह अकेली ही पैदल चलकर पसीने से तर-बतर होकर घर आती थीं। एक दिन अधिक बरसात के कारण स्कूल की गाड़ी न आने पर वह सबके मना करने पर पैदल ही स्कूल जा पहुंची थी। उसने ऐसा करके यह सिद्ध कर दिया था कि वह अकेले ही अपनी राह पर चल सकती है। वह कहती थी कि अकेलेपन का मजा ही कुछ ओर है। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व में अकेले ही अपना मार्ग बना लेने की हिम्मत थी।
![]()
HBSE 9th Class Hindi मेरे संग की औरतें Important Questions and Answers
Kritika Lesson 2 Class 9 HBSE प्रश्न 1.
लेखिका की परदादी के जीवन में ऐसे कौन-से गुण थे जिनका अनुकरण किया जाए ?
उत्तर-
लेखिका की परदादी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनके जीवन की त्याग की भावना और नारी-सम्मान की भावना विशेष रूप से अनुकरणीय थी। लेखिका की परदादी ने घोषणा कर दी थी कि वह केवल दो ही धोतियों से गुजारा करेगी। यदि तीसरी धोती मिल जाती है तो वह उसे दान कर देगी। उसने अपने पोते के यहाँ कन्या उत्पन्न होने की मन्नत माँगी थी। उसने अपनी इस मन्नत को किसी से छिपाया नहीं था। उसने अपनी इस कामना के पीछे किसी प्रकार का कोई तर्क भी नहीं दिया था। वह चाहती थी कि इस समाज में केवल लड़कों का ही नहीं, अपितु लड़कियों का भी मान-सम्मान होना चाहिए। उसकी यह भावना आज के समाज के लिए अनुकरणीय है। उसके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था थी। वह प्रभु से सदा सच्ची भावना से ही मन्नत माँगती थी जो पूरी होती थी। अतः उनके जीवन का यह गुण भी अनुकरणीय है।
Kritika Chapter 2 Mere Sang Ki Auraten HBSE प्रश्न 2.
लेखिका की माँ के जीवन के कौन-कौन से गुण आपको अत्यधिक प्रभावित करते हैं ?
उत्तर-
लेखिका की माँ एक पतली-दुबली व कमजोर-सी दिखाई देने वाली नारी थी। किंतु उनका दृढ़ निश्चय व संकल्प देखते ही बनता था। जिस काम का वह एक बार निश्चय कर लेती थी, उसे करके ही दम लेती थी। वह देशभक्त नारी थी। वह सदा ही खादी की धोती पहनती थी। लेखिका की माँ के जीवन के प्रमुख गुण थे ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्य बोलना और स्वतंत्रता-प्राप्ति के आंदोलन में भाग लेना आदि। उनके जीवन के ये वे गुण थे, जिन्हें देखकर हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और न ही कभी किसी के प्रति अन्याय होते सहन कर सकती थी। वह सदा ही देश-समाज-सेवा और त्याग को अपना धर्म मानती थी। वास्तव में लेखिका की माँ महान् विचारों वाली नारी थी।
Mere Sang Ki Auraten Prashn Uttar HBSE 9th Class प्रश्न 3.
लेखिका की नानी क्रांतिकारी विचारों वाली नारी थी। सिद्ध कीजिए।
उत्तर-
लेखिका की नानी ऊपरी तौर पर देखने में बहुत ही शांत एवं सहज लगती थी, किंतु वह सदा से नारी की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसे आज़ादी अच्छी लगती थी। भले ही वह आजादी देश की हो या व्यक्ति की। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि पति से भी खुलकर बोल पाना संभव नहीं था। किंतु उसके मन में क्रांतिकारी विचार मन-ही-मन सुलगते रहते थे। जब वह मरणासन्न थी तो उसने अपने क्रांतिकारी विचारों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। उसने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा को बुलाकर कहा कि वे उसकी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से कराएँ, किसी अंग्रेज भक्त से नहीं। यह उसके मन का अंग्रेज भक्तों के प्रति खुला विद्रोह था। इससे स्पष्ट है कि लेखिका की नानी क्रांतिकारी विचारों वाली नारी थी।
Chapter 2 Kritika Class 9 HBSE प्रश्न 4.
“हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं” इस कथन के पीछे छुपी भावना को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
यह कथन लेखिका की दादी का है। लेखिका की माँ घर के काम-काज में हाथ नहीं बँटवाती थी। वह सदा ही स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कामों में लगी रहती थी। वह बच्चों के पालन-पोषण व भरण-पोषण के काम भी नहीं करती थी। लोग जब इसका कारण पूछते कि उसे घर के काम-काज से छूट क्यों दी गई है तब लेखिका की दादी उन लोगों को उत्तर देती हुई ये शब्द कहती थी। इन शब्दों का तात्पर्य है कि लेखिका की माँ बहुत उच्च-विचारों वाली तथा देशभक्त नारी है। ये घर-गृहस्थी के काम उसके करने के योग्य नहीं हैं। इन कामों को करने के लिए हमारे पास अन्य सदस्य हैं।
Class 9th Kritika Ch 2 Question Answer HBSE प्रश्न 5.
चोर लेखिका की माँ की किस बात से प्रभावित हुआ ?
उत्तर-
चोर लेखिका की माँ के कमरे में चोरी करने के लिए घुसा था। किंतु लेखिका की माँ उससे डरी नहीं, अपितु उसे पानी लाने के लिए कहा। उसने यह भी बता दिया कि वह चोर है। फिर माँ ने कहा कि चोर हो या भगवान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोर उसे पानी देता है तथा पकड़ा जाता है। चोर लेखिका की माँ की उदारता से बहुत ही प्रभावित होता है और वह चोरी का काम छोड़कर खेती करने का काम आरंभ कर देता है।
Class 9 Kritika Chapter 2 HBSE प्रश्न 6.
स्वतंत्रता की दीवानी लेखिका 15 अगस्त, 1947 का स्वतंत्रता का समारोह देखने के लिए क्यों नहीं जा सकी थी ?
उत्तर-
लेखिका बचपन से ही स्वतंत्रता की दीवानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वह चाव से भाग लेती थी। किंतु जिस दिन स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया गया, उस दिन वह बीमार थी। उसे टाइफाइड बुखार हो गया था। उन दिनों उसे जानलेवा बुखार माना जाता था। डॉक्टर ने उसे कठोरतापूर्वक समारोह में न जाने के लिए कहा था। इसी कारण स्वतंत्रता की दीवानी लेखिका . स्वतंत्रता समारोह में न जा सकी।
![]()
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
Kritika Chapter 2 Class 9 HBSE प्रश्न 1.
‘मेरे संग की औरतें’ पाठ एक है-
(A) आत्मकथात्मक निबंध
(B) कहानी
(C) संस्मरण
(D) रिपोर्ताज
उत्तर-
(A) आत्मकथात्मक निबंध
प्रश्न 2.
‘मेरे संग की औरतें’ नामक पाठ की लेखिका का नाम है-
(A) महादेवी वर्मा
(B) मृदुला गर्ग
(C) सुभद्राकुमारी चौहान
(D) शिवरानी
उत्तर-
(B) मृदुला गर्ग
प्रश्न 3.
मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ था ?
(A) सन् 1938 में
(B) सन् 1942 में
(C) सन् 1945 में
(D) सन् 1947 में
उत्तर-
(A) सन् 1938 में
प्रश्न 4.
मूदुला गर्ग को साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली है ?
(A) कविता
(B) कथा-साहित्य
(C) निबंध
(D) नाटक
उत्तर-
(B) कथा-साहित्य
प्रश्न 5.
‘मेरे संग की औरतें’ शीर्षक पाठ किनकी समस्याओं पर आधारित है ?
(A) पुरुषों की
(B) बच्चों की
(C) बूढ़ों की
(D) औरतों की
उत्तर-
(D) औरतों की
प्रश्न 6.
लेखिका की नानी थी-
(A) परदानशी
(B) शिक्षित
(C) परंपरावादी
(D) धर्मभीरु
उत्तर-
(A) परदानशी
![]()
प्रश्न 7.
लेखिका की नानी मुँहजोर क्यों हो उठी थी ?
(A) क्रांतिकारी बनने के कारण
(B) अपनी पंद्रह वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता में
(C) परिवार की चिंता में ।
(D) पति की बेरुखी के कारण
उत्तर-
(B) अपनी पंद्रह वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता में
प्रश्न 8.
लेखिका की नानी परदे की चिंता छोड़कर किससे मिलना चाहती थी ?
(A) अपने पति से
(B) पति की माँ से
(C) पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से
(D) अपने ससुर से
उत्तर-
(C) पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से
प्रश्न 9.
लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहती थी ?
(A) जो साहबों का फरमाबरदार न हो
(B) जो कायर न हो
(C) जो सेना का सिपाही हो
(D) जो परंपरा का पालन करने वाला हो
उत्तर-
(A) जो साहबों का फरमाबरदार न हो
प्रश्न 10.
असली आजादी कब अनुभव होती है ?
(A) अपने ढंग से जीने में।
(B) संयमशीलता में
(C) आज्ञानुपालना में
(D) दूसरों को देखकर जीने में
उत्तर-
(A) अपने ढंग से जीने में
प्रश्न 11.
लेखिका की माँ का विवाह कैसे युवक से हुआ था ?
(A) जो अंग्रेजों की नौकरी करता था
(B) जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था
(C) जो कंजूस था
(D) जो माता-पिता का आज्ञाकारी पुत्र था
उत्तर-
(B) जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था
प्रश्न 12.
लेखिका की माँ ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया था ?
(A) गांधी जी के आदर्शों के कारण
(B) गरीबी के कारण
(C) आदर्श स्थापित करने के लिए .
(D) उसे अमीरों से घृणा थी
उत्तर-
(A) गांधी जी के आदर्शों के कारण
प्रश्न 13.
“हमारी बहू तो ऐसी है कि घोई, पोंछी और छींके पर टांग दी”-ये शब्द किसने, किसके लिए कहे थे ?
(A) लेखिक ने अपनी माँ के लिए
(B) लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए
(C) लेखिका की परदादी ने उसकी दादी के लिए
(D) लेखिका की सास ने उसके लिए
उत्तर-
(B) लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए
प्रश्न 14.
कौन अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे ?
(A) गांधी-नेहरू
(B) लेखिका के पिता
(C) लेखिका की नानी
(D) भारतीय जनता
उत्तर-
(A) गांधी-नेहरू
प्रश्न 15.
लेखिका की माँ की राय का कैसे पालन किया जाता था ?
(A) पत्थर की लकीर की भाँति
(B) पानी की लकीर की भाँति
(C) सख्त आदेश की भाँति
(D) राजा के फरमान की भाँति
उत्तर-
(A) पत्थर की लकीर की भाँति
![]()
प्रश्न 16.
“हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं।”-इस कथन पर बैल किसे कहा गया है ?
(A) अंग्रेजों को
(B) लेखिका की माँ को
(C) परिवार के काम करने वाले सदस्यों को
(D) स्वयं लेखिका को
उत्तर-
(C) परिवार के काम करने वाले सदस्यों को
प्रश्न 17.
‘मुस्तैद’ का अर्थ है-
(A) मस्त
(B) आलसी
(C) चालाक
(D) तत्पर
उत्तर-
(D) तत्पर
प्रश्न 18.
लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश में रुचि क्यों नहीं लेती थी ?
(A) वह बीमार रहती थी
(B) वह अधिक कमजोर थी
(C) वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण व्यस्त रहती थी
(D) उसे बच्चों से प्यार नहीं था
उत्तर-
(C) वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण व्यस्त रहती थी
प्रश्न 19.
लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय कैसे बिताती थी ?
(A) गप्पे हाँक कर
(B) सैर-सपाटे में
(C) सोने में
(D) पुस्तकें पढ़ने में
उत्तर-
D) पुस्तकें पढ़ने में
प्रश्न 20.
आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण कौन-सा है ?
(A) वह परदे में विश्वास नहीं रखती थी
(B) वह कभी झूठ नहीं बोलती थी
(C) वह दूसरों की सहायता करती थी
(D) वह दूसरों पर विश्वास करती थी
उत्तर-
(B) वह कभी झूठ नहीं बोलती थी
प्रश्न 21.
लेखिका की माँ की भूमिका बखूबी किसने निभाई थी ?
(A) लेखिका के पिता ने
(B) लेखिका की दादी ने
(C) लेखिका की बुआ ने
(D) लेखिका के दादा ने
उत्तर-
(A) लेखिका के पिता ने
प्रश्न 22.
लेखिका की परदादी की किस मन्नत के लिए लोग हैरान थे ?
(A). उसने धन के लिए मन्नत माँगी थी
(B) परिवार में लड़की के जन्म की मन्नत माँगी थी
(C) परिवार में प्रसन्नता की मन्नत माँगी थी
(D) स्वतंत्र भारत की मन्नत
उत्तर-
(B) परिवार में लड़की के जन्म की मन्नत माँगी थी
प्रश्न 23.
लेखिका की परदादी के किस व्यवहार से चोर प्रभावित हुआ था ?
(A) उदारता
(B) प्रभावशाली व्यक्तित्व
(C) उपदेश
(D) माँ-बेटे के संबंध की स्थापना से
उत्तर-
(A) उदारता
प्रश्न 24.
लेखिका के पिता ने उसे कौन-सी पुस्तक लाकर दी थी ?
(A) मेरा परिवार
(B) ब्रदर्स कारामजोव
(C) गोदान
(D) महात्मा गांधी की आत्मकथा
उत्तर-
(B) ब्रदर्स कारामजोव
प्रश्न 25.
लेखिका का भाई किस भाषा में लिखता था ?
(A) उर्दू-फारसी
(B) अंग्रेजी
(C) हिंदी
(D) अवधी
उत्तर-
(C) हिंदी
![]()
मेरे संग की औरतें Summary in Hindi
मेरे संग की औरतें पाठ-सार/गद्य-परिचय
प्रश्न-
‘मेरे संग की औरतें’ शीर्षक पाठ का सार/गद्य-परिचय अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर-
‘मेरे संग की औरतें’ एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। निबंध का सार इस प्रकार है
लेखिका की नानी उसके जन्म से पहले ही इस संसार से चल बसी थी। इसलिए लेखिका को उससे कहानी सुनने का अवसर न मिल सका। शायद इसीलिए लेखिका अपने जैसे लोगों के लिए कहानी लिखती है। लेखिका की नानी की कहानी भी बड़ी मजेदार है। उसकी नानी अनपढ़ और पर्दा-प्रथा में विश्वास करने वाली थी। उसकी शादी के तुरंत पश्चात् उसका पति उसे भारत में छोड़कर विलायत में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए चला गया। जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटा तो विलायती ढंग से भारत में रहने लगा। किंतु नानी अपने ढंग से जीवन जीती रही। उसने अपने पति की जीवन-शैली में कभी रोड़ा नही अटकाया। जब वह मरने वाली थी तो उसने अपने पति के द्वारा प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और कहा कि उनकी बेटी का विवाह किसी देशभक्त व क्रांतिकारी से करना। वह अंग्रेज़ साहबों के हुक्म का गुलाम न हो। उसकी इच्छा और स्वतंत्र विचारों को सुनकर सब दाँतों तले अंगुली देते रह गए। उसके लिए स्वतंत्रता से जीना ही बेहतर जीना था।
लेखिका की नानी की मृत्यु के पश्चात् उसकी माँ का विवाह एक ऐसे शिक्षित युवक से हुआ जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आई.सी.एस. की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। उसके पास कोई खानदानी धन भी नहीं था। इसलिए उसकी माँ को विवश होकर अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ा। वह शरीर से इतनी पतली-दुबली थी कि उसके लिए खादी की साड़ी सँभालना भी कठिन था। उसकी सास उसकी दुर्बलता का सदा मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपने ससुराल के परिवार पर बहुत दबदबा था। उसके भी दो कारण थे
(1) ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की भाँति अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का क्रांतिकारी रहा हो। किंतु घर में दबदबा अंग्रेज़ भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे क्रांतिकारी की पत्नी होना परिकथा-सा रोमांच पैदा करता था।
(2) दूसरा कारण था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व । वह सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर-दुनियादार थी। इसीलिए उसे घर के सामान्य कार्य करने के लिए भी नहीं कहा जाता था। उनकी तो केवल सलाह भर ली जाती थी, जिसका पूर्ण पालन किया जाता था। उसकी ससुराल के अन्य सदस्य ही उसकी गृहस्थी का काम सँभाले रहते थे।
लेखिका ने कभी भी अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया था। उसने न कभी अपने बच्चों को लाड़-प्यार किया और न कभी उनके लिए खाना ही बनाया तथा न ही उन्हें कभी अच्छी बहू या पत्नी होने की शिक्षा ही दी। वह घर के कामों में भी रुचि नहीं रखती थी। वह अपना अधिक समय पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। वह संगीत सुनने की भी शौकीन थी। किंतु घर के सदस्य उन्हें कभी कोई ताना नहीं देते थे। उसमें दो गुण थे-प्रथम वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। दूसरा वह एक की गोपनीय बात को सुनकर कभी दूसरों के आगे नहीं कहती थी। इसलिए बाहर के लोग भी उनके मित्र बने हुए थे। वे उस पर पूरा भरोसा रखते थे। माँ की भूमिका हमारे पिता जी ने ही निभाई थी।
लेखिका की एक परदादी भी थी। उनकी कहानी भी अजीबोगरीब है। उन्हें सदा परंपरा को तोड़ने में ही मज़ा आता था। उन्होंने मंदिर में जाकर यह मन्नत माँगी थी कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी यह घोषणा सुनकर लोग हैरान रह गए थे कि यह उसने क्या कह दिया। वे अपनी मन्नत दोहराती रही। पूरे गाँव के लोगों का विश्वास था कि उसके तार तो सीधे भगवान जी से जुड़े हुए हैं। भगवान जी ने भी उनकी ऐसी सुनी कि एक नहीं पाँच लड़कियों का जन्म हुआ।
लेखिका की परदादी के विषय में एक और घटना भी उल्लेखनीय है। एक बार घर के सभी मर्द बारात में गए हुए थे। घर की स्त्रियाँ रतजगा मना रही थीं। परदादी शोर से बचने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक चोर सेंध लगाकर उनके कमरे में आ गया। कमरे में हलचल होने से परदादी की आँख खुल गई। उसने कहा, तुम कौन हो ? चोर ने कहा जी मैं हूँ। परदादी ने कहा तुम कोई भी हो, मेरे लिए कुएँ से एक लोटा पानी का लेकर आओ। चोर ने हड़बड़ाहट में कह दिया कि मैं तो चोर हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इससे कुछ नहीं लेना-देना। बुढ़िया ने आधा लोटा पानी पीकर चोर से कहा ले आधा तू पी ले।
चोर द्वारा पानी पी लेने पर उसने कहा अब हम माँ-बेटे हुए। अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर बाहर निकलता हुआ हवेली के पहरेदारों द्वारा पकड़ा गया और माफी माँगकर बचा। उसके पश्चात् उसने चोरी करना छोड़कर खेती करना आरंभ कर दिया।
15 अगस्त, 1947 को देश को आजादी मिली। सब जगह आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। लेखिका को बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने उसे जश्न में शामिल होने को मना किया था। वह मन मसोसकर रह गई। लेखिका और उसकी अन्य चारों बहनें कभी किसी हीन-भावना की शिकार नहीं हुई थीं। लेखिका के परिवार में सभी बच्चों के दो-दो नाम थे-एक घर का और दूसरा बाहर का। लेखिका का घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला गर्ग था उसकी छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। इसी प्रकार बड़ी बहन का घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुल भगत था। उसकी दो छोटी बहनों का नाम रेणु और अचला था और भाई का नाम राजीव। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और भाई राजीव हिंदी में। रेणु का स्वभाव तो अत्यंत विचित्र था। वह गाड़ी में बैठने से इंकार कर देती और कहती थी थोड़े-से रास्ते के लिए गाड़ी में बैठना सामतंशाही का प्रतीक है। इसलिए वह पैदल ही घर पहुँचती, भले ही वह पसीने से तर-बतर हो जाती। एक बार उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मँगवाया था। इससे पूरे मुहल्ले में उसकी चर्चा हुई थी। वह तो बी०ए० की परीक्षा देना भी उचित नहीं समझती थी। जब कोई उसे इत्र भेंट करता तो तपाक से कहती, “नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ”।
![]()
तीसरे नंबर की चित्रा भी अजीब है। वह स्वयं न पढ़कर दूसरों को पढ़ाने में व्यस्त रहती। उसके अपने अंक कम आते और उसके शिष्यों के अधिक। जब शादी करने का समय आया तो उसने एक ही नज़र में लड़के को देखकर ऐलान कर दिया कि वह विवाह करेगी तो इसी से और अंत में उसी लड़के से उसका विवाह भी हो गया था।
अचला सबसे छोटी बहन है। उसने पहले एम०ए० अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और पिता की पसंद के लड़के से विवाह किया। उसे भी तीस वर्ष की आयु के पश्चात लिखने का रोग लग गया। सभी बहनों ने वैवाहिक जीवन का निर्वाह भली-भाँति किया। विवाह के पश्चात् लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए। फिर वह कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में रही। वहाँ उसने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की, किंतु अस्वीकृत हो गई। फिर लेखिका ने वहाँ अपने प्रयास से प्राइमरी स्कूल खोल दिया। रेणु लेखिका की अपेक्षा कहीं अधिक जिद्दी और बहादुर थी। वह जिस काम को करने के लिए ठान लेती, उसे करके ही दिखाती थी। एक दिन वर्षा के कारण उसके स्कूल की बस नहीं आई। वह दो कि०मी० पैदल ही स्कूल में जा पहुँची। स्कूल बंद था, उसे उसका कोई मलाल नहीं था। उसका मानना था कि अकेलेपन का मजा कुछ और ही होता है।
कठिन शब्दों के अर्थ –
(पृष्ठ-13) : जाहिर = स्पष्ट। मर्म = भेद। पारंपरिक = परंपरा से चली आ रही। परदानशी = पर्दा-प्रथा में विश्वास रखने वाली। विलायत = इंग्लैंड। बसर करना = व्यतीत करना। आकांक्षा = इच्छा।
(पृष्ठ-14) : करीब = नजदीक। इकलौती = अकेली। मुँह जोर = अधिक बोलना। लिहाज = शर्म। मर्द = पुरुष। मुँह खोलकर = बिना पर्दे के। हुजूर = दरबार। हैरतअंगेज़ = हैरान करने वाला। तय = निश्चित। फरमाबदार = आज्ञाकारी। बेखबर = अनजान होना । जुनून = पागलपन, धुन। दरअसल = वास्तव में। आजाद ख्याल = स्वतंत्र विचार। दखल देना = बाधा पहुँचाना। उबाऊ = ऊबा देने वाली, बोर। मजबूर = विवश।
(पृष्ठ-15) : अपराध = कसूर, दोष । पुश्तैनी = माँ-बाप से प्राप्त। धेला = छोटा पैसा। चनका खा जाना = मरोड़ आ जाना, नस पर नस चढ़ जाना। शर्मिंदगी = लज्जा। नाजुक = कोमल। पेशकश = कार्य के लिए आगे आना। वजह = कारण। अभिभूत = प्रभावित। शोहरत = प्रसिद्धि। दबदबा = प्रभाव। परिकथा = परियों की कहानी। सनक = जिद्द । ख्वाहिश = इच्छा। रजामंदी = मान जाना, समझौता। तिलिस्म = जादू। शख्सियत = व्यक्तित्व। नजाकत = कोमलता, अदा। परीजात = परियों की जाति। पत्थर की लकीर = अटल काम।
(पृष्ठ-16) : जुमला = कुल। ममतालू = ममता भाव से युक्त। परवरिश = देखभाल । मुस्तैद = तैयार। अरुचि = रुचि न होना। नाम धरना = चिढ़ाने के लिए गलत नाम पुकारना। रोब = प्रभाव। गोपनीय = छिपाने योग्य। बखूबी = भली-भाँति।
(पृष्ठ-17) : उबरना = मुक्त होना। निजत्व बनाना = अपना व्यक्तिगत मत या आचरण बनाना। हवाले होना = लीन होना। लीक = बँधी-बँधाई रीति। खिसके = हटे। कतार = पंक्ति। व्रत = इरादा, संकल्प। फज़ल = दया, कृपा। अपरिग्रह = एकत्रित न करना। हरकत = गलत काम। मन्नत माँगना = ईश्वर से किसी काम की कामना करना। पतोहू = पुत्रवधू। गैर-रवायती = परंपरा के खिलाफ, अप्रचलित। पोशीदा = पर्दे से ढका हुआ, छिपा हुआ। ऐलान = घोषणा। फितूर = पागलपन, सनक। वाजिब = उचित। पुश्तों = पीढ़ियों। अभाव = कमी। बदस्तूर = लगातार। मर्तबा = बार। आरजू = इच्छा। रंग लाना = प्रभाव दिखाना। गुमान = अनुमान।
(पृष्ठ-18) : गैर-वाजिब = अनुचित। जुस्तजू = चाह। अफरा-तफरी = अस्त-व्यस्त होना। नामी = प्रसिद्ध, मशहूर। दीदार = दर्शन। खुशनसीबी = अच्छा भाग्य। हाथ आना = मौका आना। रतजगा मनाना = रात को जागकर उत्सव मनाना। सेंध लगाना = चोरी से घुसना। जुगराफिया = नक्शा। पुरखिन = वृद्धा, बुढ़िया। इतमीनान = तसल्ली। टटोलकर = खोजकर। यकीन = विश्वास। धर्मसंकट = धर्म की बात सामने पाकर परेशानी में पड़ना।
(पृष्ठ-19) : अकबकाया = घबराया। एहतियात = सावधानी। धर-दबोचा = पकड़ लिया। लायक = योग्य। रोमांचक धंधा = चोरी का काम। भला मानुस = अच्छा, मनुष्य। विरासत = माँ-बाप से मिली संपत्ति। प्रकोप = गुस्सा, क्रोध। हीन भावना = कमी होने का अपराध या भाव। नाहक = व्यर्थ। रोमानी = भावना से ओत-प्रोत, संवेदनशील।
(पृष्ठ-20) : जश्न = त्योहार, समारोह। दुर्योग = बुरा अवसर। शिरकत करना = शामिल होना। इज़ाज़त = आज्ञा। सत्ताधारी = शासन करने वाले अंग्रेज़। कलपती = दुःखी होना। मिराक = मानसिक रोग। पलायन करना = चले जाना। मोहलत देना = अवकाश। गडूड-मड्ड होना = आपस में घुलमिल जाना। पल्ले पड़ना = समझ में आना। अनाचार = पापपूर्ण व्यवहार। कंठस्थ होना = याद होना।
(पृष्ठ-21) : बरकरार रखना = कायम रखना। आड़े आना = रास्ते में रुकावट बनना। पैदाइशी = जन्म से ही। नारीवाद = नारी को महत्त्व देने संबंधी आंदोलन। पोंगापंथी = पाखंडी मूर्खतापूर्ण काम करने वाला। घरघुस्सू = घर में ही घुसा रहने वाला।
![]()
(पृष्ठ-22) : तथ्य = सत्य, कथन। आलोचना-बुद्धि = अच्छे-बुरे की बातें करने वाली बुद्धि। दो-चार होना = सामना होना। नतीजतन = परिणामस्वरूप। सवा सेर होना = अधिक प्रभावी होना। आलम = हालत। सामंतशाही = बड़े-बड़े सामंतों की रईसी आदत। लाचारी = मज़बूरी। उदासीन = विमुख। कुढ़ते-भुनते = मन-ही-मन परेशान होकर बोलना। खरामा-खरामा = धीरे-धीरे। रुतबा = सम्मान, दर्जा। यकीन = विश्वास।
(पृष्ठ-23) : विश्वसनीय = विश्वास करने योग्य। कुतर्क = गलत तर्क। वाकिफ = जानकार । पेश आना = सामने आना। मुलाकात = भेंट। हथियार डालना = हार मानना।
(पृष्ठ-24) : कायम रखना = बनाए रखना। तलाक = शादी का संबंध तोड़ना। कगार = किनारा। प्रयोजन = उद्देश्य । दड़बा = समूह। अभिनय = एक्टिंग। चलन = व्यवहार। अकाल = सूखे या अधिक वर्षा के कारण अन्न न उपजना। बिशप = पादरी। इसरार = आग्रह। बशर्ते = शर्त के साथ।
(पृष्ठ-25) : सिर झुकाना = स्वीकार करना। खिसके लोग = परंपरा से हटे हुए विद्रोही लोग। व्रत = संकल्प। नमूना = उदाहरण। पेश करना = प्रस्तुत करना, देना। मुकाबिल = बराबर का। कयामती = विनाशकारी। तल्ला = मंजिल। मलाल = दुःख।
(पृष्ठ-26) : लब-लब करना = भरा-पूरा होना। निचाट = सूनापन। धुन = लगन।
HBSE 9th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 2 मेरे संग की औरतें Read More »