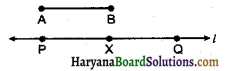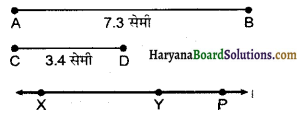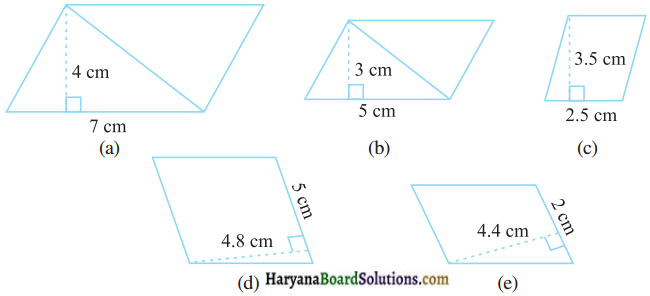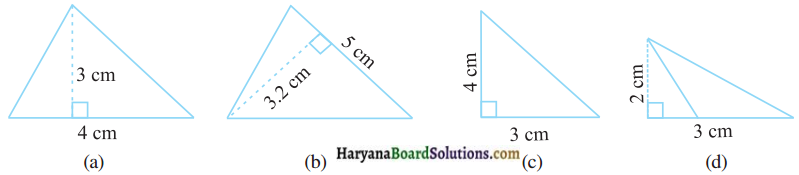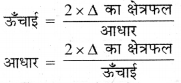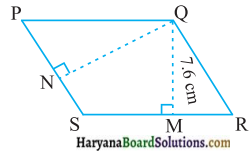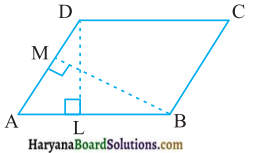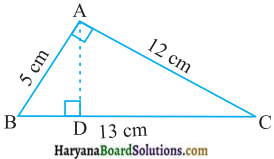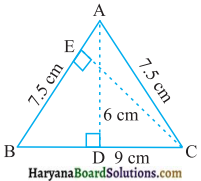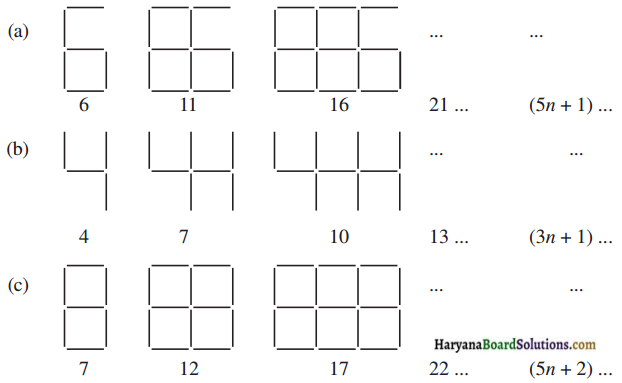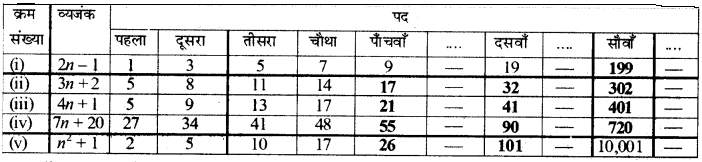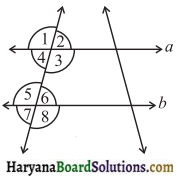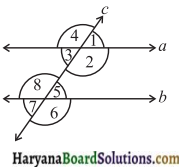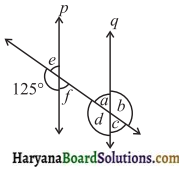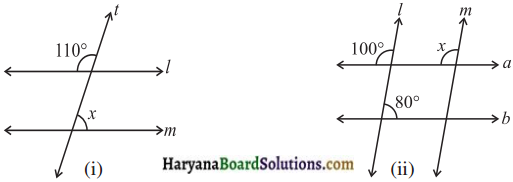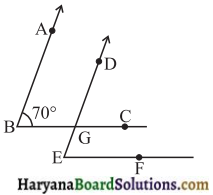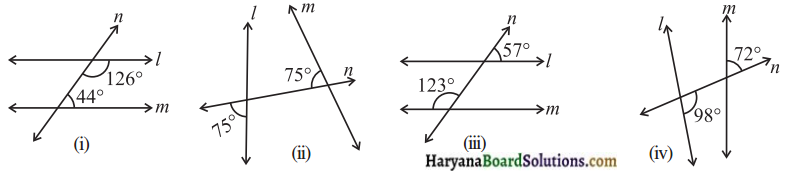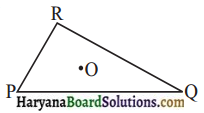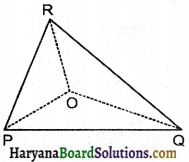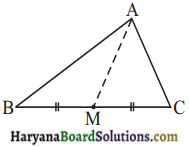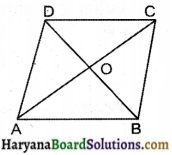Haryana State Board HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 1 मानव भूगोल : प्रकृति एवं विषय क्षेत्र Important Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Geography Important Questions Chapter 1 मानव भूगोल : प्रकृति एवं विषय क्षेत्र
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए
1. भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है?
(A) अंतर्विषयक
(B) समन्वय
(C) आंतरिक एवं समन्वय
(D) गत्यात्मक
उत्तर:
(C) आंतरिक एवं समन्वय
2. भूगोल की दो मुख्य शाखाएँ हैं-
(A) भौतिक भूगोल और मानव भूगोल
(B) क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल
(C) जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल
(D) आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल
उत्तर:
(A) भौतिक भूगोल और मानव भूगोल
3. ‘यूनिवर्सल ज्यॉग्राफी’ पुस्तक किसने लिखी?
(A) हंबोल्ट
(B) वेरेनियस
(C) बॅकल
(D) क्लूवेरियस
उत्तर:
(D) क्लूवेरियस

4. ‘ज्यॉग्राफिया जनरेलिस’ (सामान्य भूगोल) किसने लिखा?
(A) बर्नार्ड वेरेनियस
(B) हंबोल्ट
(C) चार्ल्स डार्विन
(D) कार्ल रिटर
उत्तर:
(A) बर्नार्ड वेरेनियस
5. ‘ज्यॉग्राफिया जनरेलिस’ नामक पुस्तक के दो प्रमुख भाग थे-
(A) भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल
(B) सामान्य और विशिष्ट भूगोल
(C) क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल
(D) भौतिक भूगोल और मानव भूगोल
उत्तर:
(B) सामान्य और विशिष्ट भूगोल
6. ‘ओरिजन ऑफ स्पीशीज’ पुस्तक, जो डार्विन की प्रमुख रचना है, कब प्रकाशित हुई?
(A) सन् 1870 में
(B) सन् 1859 में
(C) सन् 1856 में
(D) सन् 1854 में
उत्तर:
(B) सन् 1859 में
7. ‘ओरिजन ऑफ स्पीशीज’ (Origin of Species) नामक पुस्तक किसने लिखी?
(A) बॅकल
(B) चार्ल्स डार्विन
(C) डिमांज़िया
(D) ब्लाश
उत्तर:
(B) चार्ल्स डार्विन
8. ‘हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड’ (History of Civilization of England) नामक पुस्तक किसने लिखी?
(A) बॅकल
(B) डार्विन
(C) डिमांज़िया
(D) ब्लाश
उत्तर:
(A) बॅकल

9. ‘किताब-अल-हिन्द’ नामक ग्रंथ किसने लिखा?
(A) अलबेरूनी
(B) कार्ल रिटर
(C) जीन बूंश
(D) विडाल-डी-ला ब्लाश
उत्तर:
(A) अलबेरूनी
10. आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
(A) कार्ल रिटर
(B) रेटज़ेल
(C) जीन बूंश
(D) विडाल-डी-ला ब्लाश
उत्तर:
(B) रेटज़ेल
11. अर्ड-कुडे (Erd Kunde) नामक पुस्तक किसने लिखी?
(A) रेटजेल
(B) डिमांज़िया
(C) कार्ल रिटर
(D) क्लूवेरियस
उत्तर:
(C) कार्ल रिटर
12. ‘प्रिंसिपल्स डी ज्यॉग्राफी हयूमन’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी?
(A) बर्नार्ड वेरेनियस
(B) विडाल-डी-ला ब्लाश
(C) जीन बूंश
(D) एलन सेंपल
उत्तर:
(B) विडाल-डी-ला ब्लाश
13. भूगोल के अध्ययन के लिए ‘मानव भूगोल’ कब एक विशेष शाखा के रूप में उभरा?
(A) उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में
(B) उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में
(C) पन्द्रहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक
(D) इक्कीसवीं शताब्दी में
उत्तर:
(B) उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में
14. ‘मानव भूगोल, क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।’ यह किसने कहा?
(A) रेटजेल
(B) हंटिग्टन
(C) कुमारी सेंपल
(D) कार्ल रिटर
उत्तर:
(C) कुमारी सेंपल
15. मानव भूगोल का उद्भव कब भौगोलिक अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ? …
(A) पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में
(B) प्रारंभिक काल में
(C) बीसवीं शताब्दी में
(D) उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में
उत्तर:
(D) उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में
16. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है?
(A) व्यावहारिक भूगोल
(B) सामाजिक भूगोल
(C) राजनीतिक भूगोल
(D) भौतिक भूगोल
उत्तर:
(D) भौतिक भूगोल
17. मानव भूगोल एक मुख्य शाखा है-
(A) क्रमबद्ध भूगोल की
(B) प्रादेशिक भूगोल की
(C) भौतिक भूगोल की
(D) पर्यावरण भूगोल की
उत्तर:
(A) क्रमबद्ध भूगोल की

18. “मनुष्य प्रकृति का दास है” यह कथन भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है?
(A) निश्चयवाद
(B) संभावनावाद
(C) संभववाद
(D) व्यवहारदाद
उत्तर:
(A) निश्चयवाद
19. निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे-
(A) जर्मन भूगोलवेत्ता
(B) फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता
(C) अमेरिकन भूगोलवेत्ता
(D) रोमन भूगोलवेत्ता
उत्तर:
(A) जर्मन भूगोलवेत्ता
20. नव नियतिवाद के प्रवर्तक थे-
(A) हंबोल्ट
(B) विडाल-डी-ला ब्लाश
(C) ग्रिफिथ टेलर
(D) रेटजेल
उत्तर:
(C) ग्रिफिथ टेलर
21. मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लूसियन फ्रेबने और विडाल-डी-ला ब्लाश ने किस विचारधारा का अनुसरण किया था?
(A) निश्चयवाद
(B) संभावनावाद
(C) संभववाद
(D) प्रत्यक्षवाद
उत्तर:
(C) संभववाद
22. किस तत्त्व को ‘माता प्रकृति’ कहते हैं?
(A) भौतिक पर्यावरण
(B) सांस्कृतिक पर्यावरण
(C) राजनीतिक पर्यावरण
(D) औद्योगिक पर्यावरण
उत्तर:
(A) भौतिक पर्यावरण
23. व्यवहारवाद किसने प्रतिपादित किया?
(A) ग्रिफिथ टेलर
(B) जीन बूंश
(C) गेस्टाल्ट संप्रदाय
(D) डिमांज़िया
उत्तर:
(C) गेस्टाल्ट संप्रदाय
24. निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद के समर्थक नहीं थे?
(A) बी. जे. एल. बैरी
(B) विलियम बंग
(C) हंटिंग्टन
(D) डेविड हार्वे
उत्तर:
(C) हंटिंग्टन
25. कल्याणपरक विचारधारा के समर्थक थे-
(A) बैरी, विलियम बंग
(B) गेस्टाल्ट संप्रदाय
(C) डी. एम. स्मिथ, डेविड हार्वे
(D) ईसा बोमेन
उत्तर:
(C) डी. एम. स्मिथ, डेविड हार्वे

26. ‘कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे?’ यह वाक्य किस विचारधारा का मूलबिंदु है?
(A) निश्चयवाद
(B) प्रत्यक्षवाद
(C) कल्याणपरक
(D) व्यवहारवाद
उत्तर:
(C) कल्याणपरक
B. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए
प्रश्न 1.
‘यूनिवर्सल ज्यॉग्राफी’ पुस्तक किसने लिखी?
उत्तर:
क्लूवेरियस ने।
प्रश्न 2.
‘ओरिजन ऑफ स्पीशीज’ पुस्तक, जो डार्विन की प्रमुख रचना है, कब प्रकाशित हुई?
उत्तर:
वर्ष 1859 में।
प्रश्न 3.
‘एंथ्रोपोज्यॉग्राफी’ नामक ग्रंथ किसने लिखा?
उत्तर:
जर्मनी के रेटजेल ने।
प्रश्न 4.
निश्चयवाद के प्रबल समर्थक कौन थे?
उत्तर:
फ्रेडरिक रेटज़ेल।
प्रश्न 5.
‘Principles de Geographie Humaine’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी?
उत्तर:
विडाल-डी-ला ब्लाश ने।
प्रश्न 6.
मानव भूगोल किसकी मुख्य शाखा है?
उत्तर:
क्रमबद्ध भूगोल।
प्रश्न 7.
व्यवहारवाद किसने प्रतिपादित किया?
उत्तर:
गेस्टाल्ट संप्रदाय ने।
प्रश्न 8.
‘कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे?’ यह वाक्य किस विचारधारा का मूल-बिंदु है?
उत्तर:
कल्याणपरक विचारधारा का।
प्रश्न 9.
“मनुष्य प्रकृति का दास है।” यह कथन भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है?
उत्तर:
निश्चयवाद विचारधारा से।

प्रश्न 10.
आधुनिक मानव भूगोल का जनक अथवा संस्थापक किसे कहा जाता है?
उत्तर:
फ्रेडरिक रेटज़ेल को।
प्रश्न 11.
नव-निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे?
उत्तर:
ग्रिफ़िथ टेलर।
प्रश्न 12.
रेटज़ेल कहाँ के भूगोलवेत्ता थे?
उत्तर:
जर्मनी के।
अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
मानव भूगोल क्या है?
अथवा
रेटज़ेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा लिखें।
उत्तर:
मानव भूगोल वह विषय है जो प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय जगत् के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। रेटज़ेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।”
प्रश्न 2.
कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए।
उत्तर:
कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल के अनुसार, “मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।”
प्रश्न 3.
आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक वातावरण आदि के साथ मनुष्य के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समुदाय जीवन-यापन के लिए भिन्न-भिन्न साधन अपनाता है; जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, आखेट, कृषि, खनन, भोज्य पदार्थ, व्यवसाय आदि।

प्रश्न 4.
फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोज्यॉग्राफी का प्रकाशन एक युगांतकारी घटना क्यों कहलाती है?
उत्तर:
इस पुस्तक ने भूगोल में मानव केन्द्रित विचारधारा को स्थापित किया। रेटज़ेल ने मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया।
प्रश्न 5.
प्रौद्योगिक स्तर मनुष्य व प्रकृति के आपसी संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है?
उत्तर:
जब मनुष्य उपकरणों व तकनीकों की सहायता से निर्माण कार्य करता है तो वह प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्रकृति के नियमों को ठीक प्रकार से समझकर व प्रौद्योगिकी का विकास करके मानव निर्माण का कार्य करता है; जैसे तेज गति से चलने वाले यान वायुगति के नियमों पर आधारित होते हैं।
प्रश्न 6.
भौतिक भूगोल किसे कहते हैं?
उत्तर:
भौतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्त्वों का अध्ययन करता है अर्थात् इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 7.
प्रौद्योगिकी को विकसित करने में प्रकृति का ज्ञान क्यों अनिवार्य है?
उत्तर:
क्योंकि सभी उपकरणों की कार्यविधि और तकनीकों को हम प्रकृति से सीखते हैं।
प्रश्न 8.
मानव का प्रकृतिकरण अथवा प्राकृतिक मानव से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
प्रौद्योगिकी-विहीन आदिम लोगों द्वारा जीवन जीने के लिए प्रकृति पर प्रत्यक्ष एवं पूर्ण निर्भरता मानव का प्रकृतिकरण कहलाती है।
प्रश्न 9.
प्रकृति के मानवीकरण अथवा मानवकृत प्रकृति से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
अपनी बुद्धि और कौशल इत्यादि के बल पर विकसित प्रौद्योगिकी के द्वारा मनुष्य का प्रकृति पर छाप छोड़ना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है।
प्रश्न 10.
अध्ययन की विधि के आधार पर भूगोल की कौन-सी दो शाखाएँ हैं?
उत्तर:
- क्रमबद्ध भूगोल (Systematic Geography)
- प्रादेशिक भूगोल (Regional Geography)।
प्रश्न 11.
फ्रांस के किन्हीं चार मानव भूगोलवेत्ताओं के नाम बताएँ।
उत्तर:
- विडाल-डी-ला ब्लाश
- जीन बूंश
- हम्बोल्ट
- कार्ल रिटर।
प्रश्न 12.
भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्त्व कौन-से हैं?
उत्तर:
भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्त्व-मृदा, जलवायु, भू-आकृति, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी-जातियाँ तथा वनस्पति-जातियाँ आदि हैं।

प्रश्न 13.
राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र बताइए।
उत्तर:
- निर्वाचन भूगोल
- सैन्य भूगोल।
प्रश्न 14.
आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र बताइए।
उत्तर:
- संसाधन भूगोल
- कृषि भूगोल
- उद्योग भूगोल
- विपणन भूगोल
- पर्यटन भूगोल
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल।
प्रश्न 15.
समायोजन से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक दशाओं और संसाधनों के अनुसार मानव द्वारा चयनित व्यवसाय को प्रकृति के साथ समायोजन कहते हैं।
प्रश्न 16.
पर्यावरण से क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
पर्यावरण शब्द हिन्दी के दो पदों परि + आवरण के मेल से बना है। ‘परि’ का अर्थ है-‘चारों ओर से’ तथा आवरण का अर्थ है-‘ढके हुए’ अर्थात् पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है।
प्रश्न 17.
पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है?
उत्तर:
पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य तुच्छ, शक्तिहीन एवं निष्क्रिय होता है।
प्रश्न 18.
निश्चयवाद क्या है?
उत्तर:
मानव-शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन निश्चयवाद कहलाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव-जीवन और उसके व्यवहार को विशेष रूप से भौतिक वातावरण के तत्त्व प्रभावित और यहाँ तक कि निर्धारित करते हैं।
प्रश्न 19.
मानव-पर्यावरण सम्बन्धों की व्याख्या करने वाली तीन अवधारणाओं के नाम लिखें।
उत्तर:
- नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद
- सम्भववाद
- नव-निश्चयवाद।

प्रश्न 20.
मानव भूगोल के दो प्रमुख उद्देश्य कौन-से हैं?
उत्तर:
मानव भूगोल यह जानने का प्रयत्न करता है कि-
- मानव ने किन-किन प्रदेशों में क्या-क्या विकास किया है-रचनात्मक या विध्वंसात्मक।
- मानव और वातावरण के बीच ऐसे कौन-से संबंध हैं जिनके फलस्वरूप समस्त विश्व एक पार्थिव एकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है।
प्रश्न 21.
भूगोल पृथ्वी तल पर विस्तृत किन दो प्रकार के तत्त्वों का अध्ययन करता है?
उत्तर:
भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी तत्त्वों को दो वर्गों में बाँटता है-
- भौतिक तत्त्व
- मानवीय तत्त्व।
भौतिक तत्त्वों की रचना प्रकृति करती है। इनकी रचना में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। मानवीय तत्त्वों का निर्माण स्वयं मनुष्य करता है, लेकिन उनका आधार भौतिक तत्त्व ही होते हैं।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय कैसे है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय है। जिस प्रकार तकनीक के विकास के साथ मनुष्य और पर्यावरण का सम्बन्ध बदलता जा रहा है, उसी प्रकार मानव भूगोल की विषय-वस्तु में भी समय के साथ विस्तार होता जा रहा है। उदाहरणतया बीसवीं सदी के आरंभ में मानव भूगोल में सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाता था किंतु बाद में नई समस्याओं और चुनौतियों के आने पर उन्हें भी विषय-वस्तु का अंग बना लिया गया। वर्तमान में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक आयाम, सामाजिक संबद्धता, लिंग असमानता, जन-नीति, नगरीकरण तथा नगर प्रणाली, स्वास्थ्य व सामाजिक सुविधाएँ इत्यादि प्रकरणों को शामिल किया गया।
प्रश्न 2.
जीन बूंश द्वारा बताए गए मानव भूगोल के आवश्यक तत्त्वों का उल्लेख करें।
उत्तर:
जीन बूंश ने मानव भूगोल की विषय-वस्तु को पाँच प्रकार के आवश्यक तथ्यों के अध्ययन के रूप में विभाजित किया है जो इस प्रकार हैं-
- मृदा के अनुत्पादक व्यवसाय से संबंधित तथ्य; जैसे मकान और सड़कें
- वनस्पति और जीव-जगत् पर मानव विजय से संबंधित तथ्य; जैसे कृषि
- पशुपालन
- पशुपालन और मृदा के विनाशकारी उपयोग से संबंधित तथ्य; जैसे पौधों और पशुओं का विनाश
- खनिजों का अवशोषण।
प्रश्न 3.
मानव भूगोल की विषय-वस्तु अथवा अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किन्हीं चार प्रमुख तथ्यों की चर्चा कीजिए।
उत्तर:
मानव भूगोल की विषय-वस्तु के अंतर्गत मोटे तौर पर निम्नलिखित चार तथ्यों का अध्ययन किया जाता है-
- मानव का उद्गम, उसकी प्रजातियाँ तथा भूमंडल पर मानव प्रजातियों का देशकालीन (Spatio-temporal) स्थापन।
- जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, घनत्व, जनांकिकीय विशेषताएँ तथा प्रवास एवं मिश्रण।
- मानव की नितांत आवश्यकताएँ-भोजन, वस्त्र और मकान।
- भू-आकारों, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल, जीवों व खनिजों से संबंध व समायोजन।

प्रश्न 4.
निश्चयवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:
मानव-शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन निश्चयवाद कहलाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव-जीवन और उसके व्यवहार को विशेष रूप से भौतिक वातावरण के तत्त्व प्रभावित व निर्धारित करते हैं अर्थात मानवीय क्रियाओं पर वातावरण का नियन्त्रण होता है। इसके अनुसार किसी सामाजिक वर्ग की सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, रहन-सहन तथा विकासात्मक पक्ष भौतिक कारकों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव एक क्रियाशील कारक नहीं है। इस विचारधारा को यूनानी तथा रोमन विद्वानों हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस तथा स्ट्रेबो ने प्रस्तुत किया। इसके बाद अल-मसूदी, अल-अदरीसी, काण्ट, हम्बोल्ट तथा रेटज़ेल आदि ने इस पर विशेष कार्य किया। अमेरिका में कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल तथा ए० हंटिंग्टन ने इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया।
प्रश्न 5.
क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर:
क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में निम्नलिखित अंतर हैं-
| क्रमबद्ध भूगोल | प्रादेशिक भूगोल |
| 1. क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्त्व का अध्ययन होता है। | 1. प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्त्चों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। |
| 2. क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन का एकाकी (Isolated) रूप प्रस्तुत करता है। | 2. प्रादेशिक भूगोल अध्ययन का समाकलित (Integrated) रूप प्रस्तुत करता है। |
| 3. क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। | 3. प्रादेशिक भूगोल में अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। |
| 4. क्रमबद्ध भूगोल किसी तत्च विशेष के क्षेत्रीय वितरण, उसके कारणों और प्रभावों की समीक्षा करता है। | 4. प्रादेशिक भूगोल किसी प्रदेश विशेष के सभीं भौगोलिक तत्त्वों का अध्ययन करता है। |
| 5. क्रमबद्ध भूगोल में किसी घटक; जैसे जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या वर्षा की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार और उप-प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। | 5. ‘प्रादेशिक भूगोल में प्राकृतिक तत्त्चों के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण की यह प्रक्रिया प्रादेशीकरण (Regionalisation) कहलाती है। |
प्रश्न 6.
भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर:
भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में निम्नलिखित अंतर हैं
| भौतिक भूगोल | मानव भूगोल |
| 1. भौतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्त्वों का अध्ययन करता है। | 1. मानव भूगोल पृथ्वी तल पर फैली मानव-निर्मित परिस्थितियों का अध्ययन करता है। |
| 2. भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। | 2. मानव भूगोल में मनुष्य के सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। |
प्रश्न 7.
सांस्कृतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं?
अथवा
सामाजिक भूगोल से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
भूगोल के अन्तर्गत मनुष्य के सांस्कृतिक पहलुओं; जैसे मानव का आवास, सुरक्षा, भोजन, रहन-सहन, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, पहनावा आदि का अध्ययन किया जाता है। भिन्न-भिन्न मानव समुदायों की कला, तकनीकी उन्नति और विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित होना मोटे तौर पर उनके भौगोलिक पर्यावरण की देन है। कुछ भूगोलवेत्ता सांस्कृतिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। सामाजिक भूगोल में मानव को एकाकी रूप में न लेते हुए मानव समूहों और पर्यावरण के सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है। सांस्कृतिक भूगोल में भिन्न-भिन्न मानव समुदायों के सांस्कृतिक विकास तथा उसके पर्यावरण के आपसी सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है।
प्रश्न 8.
निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर:
निश्चयवाद और संभववाद में निम्नलिखित अंतर हैं-
| निश्चयवाद | संभववाद |
| 1. निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। | 1. संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। |
| 2. इस विचारधारा के समर्थक रेटज़ेल, हम्बोल्ट व हंटिंग्टन थे। | 2. इस विचारधारा के समर्थक विडाल-डी-ला ब्लाश और फ्रैबवे थे। |
| 3. यह एक जर्मन विचारधारा है। | 3. यह एक फ्रांसीसी विचारधारा है। |
प्रश्न 9.
कृषि भूगोल से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
मानव भूगोल की इस शाखा या उपक्षेत्र में कृषि सम्बन्धी सभी तत्त्वों; जैसे कृषि भूमि, सिंचाई, कृषि उत्पादन तथा पशुपालन व पशु उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। कृषि से मनुष्य की मूलभूत जरूरत ‘भोजन’ की आपूर्ति होती है। इसलिए मानव भूगोल की यह शाखा या उपक्षेत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इन शाखाओं के अतिरिक्त मानव भूगोल की कई अन्य उपशाखाएँ; जैसे नगरीय भूगोल (Urban Geography), अधिवास भूगोल (Settlement Geography), चिकित्सा भूगोल (Medical Geography), व्यापारिक भूगोल (Commercial Geography), ग्रामीण भूगोल (Rural Geography), औद्योगिक भूगोल (Industrial Geography) तथा व्यावहारिक भूगोल (Applied Geography) आदि हैं।
प्रश्न 10.
संभववाद से आप क्या समझते हैं?
अथवा
संभववाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
उत्तर:
सम्भववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक पॉल विडाल-डी-ला ब्लाश थे। उनके पश्चात् अन्य भूगोलवेत्ताओं ब्रूश, डिमांजियां आदि ने भी इस विचारधारा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सम्भववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्रैबवे ने किया था जो ब्लाश के दृष्टिकोण पर आधारित था।
इस विचारधारा के अनुसार, प्रकृति के द्वारा कुछ सम्भावनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनके अन्दर मानव की छाँट द्वारा किसी क्षेत्र के साथ मानव समाज अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इन भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा फ्रांस में तथा संसार के अन्य देशों में भी मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भू-दृश्य का वर्णन करते हुए दर्शाया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए मानवीय छाँट ही महत्त्वपूर्ण होती है। किसी प्रदेश की स्थिति और जलवायु से अधिक महत्त्वपूर्ण मानव होता है और मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक भी होता है।

प्रश्न 11.
नव-निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
ग्रिफिथ टेलर ने नव-निश्चयवाद को समझाने के लिए “रुको तथा जाओ” वाक्यांश का प्रयोग किया। उनके अनुसार, मनष्य पर प्रकति का प्रभाव पड़ता है परन्त मनुष्य में भी अपने बद्धि-कौशल तथा प्रौद्योगिकी के दम पर प्रकृति को बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मनुष्य अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रकृति का उपयोग भी कर सकता है। इसी विचारधारा को नव-निश्चयवाद कहा जाता है।
प्रश्न 12.
नियतिवाद या वातावरण निश्चयवाद पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
नियतिवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ। हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत के अनुसार, मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। रेटजेल के अनुसार, मानव अपने वातावरण की उपज है। वातावरण ही मानव के जीवन-यापन के ढंग अर्थात् भोजन, वस्त्र, मकान और सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। मनुष्य केवल वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं को वहाँ रहने योग्य बनाता है।
टुंड्रा के एस्किमो, जायरे बेसिन के पिग्मी व कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन आदि कबीलों ने आखेट द्वारा जीवन-यापन को स्वीकार कर भौतिक परिवेश में समायोजित हो गए। हम्बोल्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘कॉसमॉस’ में वातावरण के प्रभावों का स्पष्ट आभास मिलता है। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों को मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों पर और मनुष्यों के रहन-सहन पर स्पष्टतः प्रदर्शित किया था।
दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए।
अथवा
मानव भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है? मानव भूगोल की प्रकृति का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Human Geography)-विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल को अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं
1. फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है।”
2. कुमारी सेम्पल के अनुसार, “मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।”
3. पॉल विडाल-डी-ला ब्लाश के अनुसार, “हमारी पृथ्वी को नियन्त्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य सम्बन्धों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं।”
4. एल्सवर्थ हंटिंग्टन के अनुसार, “मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानव के क्रियाकलापों एवं गुणों के सम्बन्ध . के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है।”
5. जीन बूंश के अनुसार, “मानव भूगोल उन सभी वस्तुओं का अध्ययन है जो मानव क्रियाकलाप द्वारा प्रभावित है और जो हमारी पृथ्वी के धरातलीय पदार्थों की एक विशेष श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं।”
6. कैकिले वैलो के अनुसार, “मानव भूगोल वह विज्ञान है जो विस्तृत अर्थों में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है।”
7. ए० डिमांजियां के अनुसार, “मानव भूगोल समुदायों तथा समाज के भौतिक वातावरण से सम्बन्धों का अध्ययन है।”
अतः मानव भूगोल के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में बसा मानव अपने वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित कर उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करता है। मानव भूगोल एक दर्शनशास्त्र के समान है। मनुष्य की विचारधारा और जीवन-दर्शन पर किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उस पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन नहीं है। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है, जिसमें भूतल के विभिन्न भागों के रहने वाले मानव समूहों तथा उनसे उत्पन्न तथ्यों या भू-दृश्यों का अध्ययन किया जाता है।
मानव भूगोल की प्रकृति (Nature of Human Geography):
मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य तथा वातावरण के बीच पारस्परिक कार्यात्मक सम्बन्धों (Functional Relations) का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति को उसके अर्थ तथा परिभाषाओं के द्वारा जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से मानव भूगोल का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मानव भूगोल में भौतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी पर फैली मानव सभ्यता द्वारा निर्मित परिस्थितियों तथा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। घर, खेत, गाँव, नहरें, पुल, सड़कें, नगर, कारखाने, बाँध व स्कूल इत्यादि मानवीय लक्षणों के उदाहरण हैं।
वास्तव में, फ्रांस के पॉल विडाल-डी-ला ब्लाश (Paul Vidal-de-la Blache) तथा जीन बूंश (Jean Brunches) ने मानव भूगोल को अत्यधिक महत्त्व देकर उसे उच्च शिखर पर बिठा दिया है। प्राकृतिक दशाओं के आधार पर मानव भूगोल के तत्त्वों को आसानी से समझा भी जा सकता है। मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक सम्बन्धों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच सतत् परिवर्तनशील क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 2.
भूगोल का मानव एवं वातावरण के साथ संबंध का दो प्रमुख उपागमों के अंतर्गत वर्णन कीजिए।
अथवा
मानव भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागमों-नियतिवाद और संभववाद का विस्तृत वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भौगोलिक अध्ययन के कई पक्ष होते हैं, परंतु भूगोल में मानव और वातावरण के संबंधों को लेकर दो पृथक विचारधाराएँ विकसित हुईं। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में मानव और वातावरण के सम्बन्धों का विस्तृत अध्ययन किया गया जिसमें वातावरण को सर्वप्रमुख माना गया। तत्पश्चात् इस विचारधारा में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानवीय पक्ष को प्रधानता दी। ये विचारधाराएँ निम्नलिखित हैं
1. नियतिवाद या वातावरण निश्चयवाद (Environmental Determinism) – नियतिवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ। हम्बोल्ट, रिटर और रेटज़ेल इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत के अनुसार, मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। रेटजेल के अनुसार, मानव अपने वातावरण की उपज है। वातावरण ही मानव के जीवन-यापन के ढंग अर्थात् भोजन, वस्त्र, मकान और सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। मनुष्य केवल वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं को वहाँ रहने योग्य बनाता है। टुंड्रा के एस्किमो, जायरे बेसिन के पिग्मी व कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन आदि कबीलों ने आखेट द्वारा जीवन-यापन को स्वीकार कर भौतिक परिवेश में समायोजित हो गए। हम्बोल्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘कॉसमॉस’ में वातावरण के प्रभावों का स्पष्ट आभास मिलता है। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों को मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों पर और मनुष्यों के रहन-सहन पर स्पष्टतः प्रदर्शित किया था।
आलोचना (Criticism) – यह बात सत्य है कि वातावरण मनुष्य को प्रभावित करता है परंतु मनुष्य भी वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। यह पारस्परिक क्रिया इतनी गहन है कि यह जानना कठिन होता है कि किस समय एक क्रिया का प्रभाव बंद होता है और दूसरी क्रिया का प्रभाव आरंभ होता है। समान भौतिक परिवेश वाले क्षेत्रों में विकास के स्तर में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। पृथ्वी तल पर जनसंख्या के वितरण में जो विषमताएँ पाई जाती हैं उनका कारण केवल वातावरण ही नहीं है। बहुत-से भू-दृश्य जो हमें प्राकृतिक प्रतीत होते हैं वे वास्तव में मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अतः नियतिवाद की इस आधार पर आलोचना की गई कि जहाँ पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, वहाँ मानव भी पर्यावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है।
2. संभववाद (Possibilism)-संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक विडाल-डी-ला ब्लाश थे। उनके पश्चात् अन्य भूगोलवेत्ताओं जीन ब्रश, डिमांजियां आदि ने भी इस विचारधारा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्रॅबवे ने किया
था जो ब्लाश के दृष्टिकोण पर आधारित था।
इस विचारधारा के अनुसार, प्रकृति के द्वारा कुछ संभावनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनके अंदर मानव की छाँट (Human Choice) द्वारा किसी क्षेत्र के साथ मानव समाज अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इन भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा फ्रांस में तथा संसार के अन्य देशों में भी मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भू-दृश्य का वर्णन करते हुए दर्शाया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ते के लिए मानवीय छाँट ही महत्त्वपूर्ण होती है। किसी प्रदेश की स्थिति और जलवायु से अधिक महत्त्वपूर्ण मानव होता है और मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है।
निष्कर्ष (Conclusion) – यद्यपि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है फिर भी प्रभाव अवश्य है और मानव उस प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही विकास कर सकता है। वास्तव में, न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक-दूसरे से क्रियात्मक सम्बन्ध है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति के साथ सहयोगी बनकर रहे।

प्रश्न 3.
“द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात, मानव भूगोल ने मानव समाज की समकालीन समस्याओं और चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए।” इस कथन की विवेचना कीजिए।
अथवा
मानव भूगोल के अध्ययन की विभिन्न विधियों या उपागमों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
उत्तर:
द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् भूगोल में विशेषीकरण की प्रवृत्ति आ गई। इस समय भूगोल के अंतर्गत बस्तियाँ, नगर, बाजार, मनोरंजन, सैन्य भूगोल, प्रादेशिक असमानता, गरीबी, लिंग भेद, निरक्षरता आदि संवेदनशील उपविषय पढ़े जा रहे हैं। ये सभी विषय मूल रूप से मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं लेकिन समकालीन मुद्दों और समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान ढूँढने में पारंपरिक विधियां असमर्थ हैं। फलस्वरूप मानव भूगोल ने समय-समय पर अनेक नई विधियों को अपनाया जो समकालीन समस्याओं और चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती हैं। इस उद्देश्य के लिए मानव भूगोल में अपनाई गई विधियाँ अग्रलिखित हैं-
1. प्रत्यक्षवाद (Positivism) इसमें मात्रात्मक विधियों पर अधिक बल दिया गया जिससे भौगोलिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। इस विचारधारा की प्रमुख कमी यह थी कि इसमें मानवीय गुणों; जैसे धैर्य, क्षमता, विश्वास आदि का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।
2. व्यवहारवाद (Behaviouralism)-इस विचारधारा के अनुसार, संपूर्ण अपने अंश अथवा अवयवों से महत्त्वपूर्ण होता है। अतः परिस्थिति का समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया जाना चाहिए। इस विधि में मानव अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करके समस्याओं का बौद्धिक हल ढूँढ सकता है।
3. कल्याणपरक विचारधारा (Welfare Approach) विश्व में व्याप्त विभिन्न प्रकार की असमानताओं की प्रतिक्रियास्वरूप मानव भूगोल में कल्याणपरक प्रतिक्रिया का जन्म हुआ। इसमें निर्धनता, बेरोज़गारी, प्रादेशिक असंतुलन, नगरीय झुग्गी-झोंपड़ियाँ तथा आर्थिक असमानता जैसे विषयों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया।
4. मानवतावाद (Humanism)-मानवतावाद मनुष्य की सूजन शक्ति पर आधारित मानव भूगोल की एक नवीन विचारधारा है। इसमें मानव जागृति, मानव संसाधन तथा उसकी सृजनात्मकता के संदर्भ में मनुष्य की सक्रिय भूमिका का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 4.
मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं या उपक्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल की शाखाएँ या उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं-
1. आर्थिक भूगोल (Economic Geography) – आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की सबसे प्रमुख शाखा है। आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक वातावरण आदि के साथ मनुष्य के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समुदाय जीवन-यापन के लिए भिन्न-भिन्न साधन अपनाता है; जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, आखेट, कृषि, खनन, भोज्य पदार्थ, व्यवसाय आदि। आर्थिक भूगोल भू-पृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के विभिन्न तत्त्वों; जैसे मिट्टी, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति,. खनिज संसाधन, जनसंख्या तथा घनत्व आदि का प्रभाव पड़ता है।
2. सांस्कृतिक भूगोल (Cultural Geography) – मानव भूगोल की इस शाखा के अन्तर्गत मनुष्य के सांस्कृतिक पहलुओं; जैसे मानव का आवास, सुरक्षा, भोजन, रहन-सहन, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, पहनावा आदि का अध्ययन किया जाता है। भिन्न-भिन्न मानव समुदायों की कला, तकनीकी उन्नति और विज्ञान के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित होना मोटे तौर पर उनके भौगोलिक पर्यावरण
की देन है। कुछ भूगोलवेत्ता सांस्कृतिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। सामाजिक भूगोल में मानव को एकाकी रूप न लेते हुए मानव समूहों और पर्यावरण के सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है। सांस्कृतिक भूगोल में भिन्न-भिन्न मानव समुदायों के सांस्कृतिक विकास तथा उसके पर्यावरण के आपसी सम्बन्धों की व्याख्या की जाती है।
3. ऐतिहासिक भूगोल (Historical Geography) – मानव भूगोल की इस शाखा में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। ऐतिहासिक भूगोल विश्लेषण करता है कि किस प्रकार धरातल, स्थिति, भौगोलिक एकान्तता, प्राकृतिक बाधाएँ तथा राज्य का विस्तार
आदि किसी राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करती है। हार्टशान के अनुसार, “ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है।”
4. राजनीतिक भूगोल (Political Geography) – मानव भूगोल की इस शाखा के अन्तर्गत राष्ट्रों या राज्यों की सीमाएँ, विस्तार, स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक नियोजन आदि आते हैं। राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल मानवीय समूहों की राजनीतिक परिस्थितियों, समस्याओं व क्रियाओं से भूगोल के महत्त्व को प्रदर्शित करता है। राजनीतिक भूगोल राज्यों का भूगोल है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत करता है।
5. सैन्य भूगोल (Military Geography) – मानव भूगोल की इस शाखा के अन्तर्गत स्थल तथा समुद्र के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करना है। इस भूगोल में युद्ध के स्थानों के निर्धारण के लिए सम्बन्धित क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं, स्थिति, जलाशयों, उच्चावच, जंगली भूमि आदि की जानकारी आवश्यक होती है। इस भूगोल में अध्ययन के लिए मानचित्रों तथा स्थलाकृतिक मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है।
6. कृषि भूगोल (Agricultural Geography) – मानव भूगोल की इस शाखा या उपक्षेत्र में कृषि सम्बन्धी सभी तत्त्वों; जैसे कृषि भूमि, सिंचाई, कृषि उत्पादन तथा पशुपालन व पशु उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। कृषि से मनुष्य की मूलभूत जरूरत ‘भोजन’ की आपूर्ति होती है। इसलिए मानव भूगोल की यह शाखा या उपक्षेत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इन शाखाओं के अतिरिक्त मानव भूगोल की कई अन्य उपशाखाएँ; जैसे नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यापारिक भूगोल, ग्रामीण भूगोल, औद्योगिक भूगोल तथा व्यावहारिक भूगोल आदि हैं।
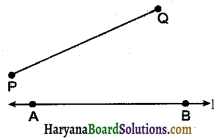
![]()