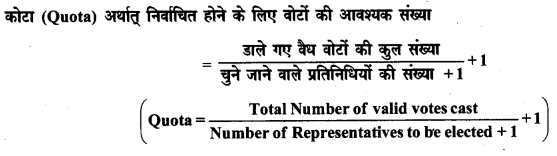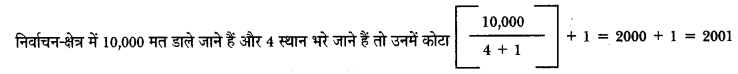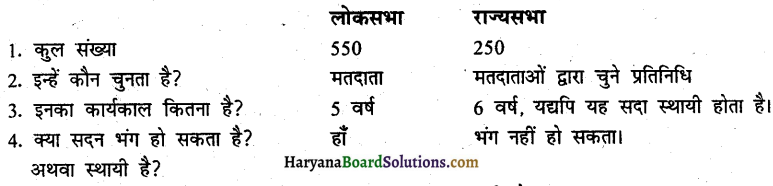Haryana State Board HBSE 12th Class Sociology Important Questions Chapter 2 सांस्कृतिक परिवर्तन Important Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Sociology Important Questions Chapter 2 सांस्कृतिक परिवर्तन
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. भारत को धर्म निष्पक्षता किसने प्रदान की है?
(A) राज्य
(B) सरकार
(C) जनता
(D) संविधान।
उत्तर:
संविधान।
2. उस देश को क्या कहते हैं जो किसी विशेष धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है?
(A) कल्याणकारी राज्य
(B) धर्म निष्पक्ष
(C) लोकतांत्रिक
(D) तानाशाही।
उत्तर:
धर्म निष्पक्ष।
3. इनमें से कौन-सा धर्म निष्पक्षता का आवश्यक तत्त्व है?
(A) धार्मिक कट्टरवाद का बढ़ना
(B) धार्मिक गतिविधियों का बढ़ना
(C) धार्मिक कट्टरवाद का खात्मा
(D) धार्मिक गतिविधियां का खात्मा।
उत्तर:
धार्मिक कट्टरवाद का खात्मा।

4. इनमें से कौन-सा धर्म निष्पक्षता का मुख्य आधार है?
(A) धर्म
(B) तार्किकता तथा विज्ञान
(C) धार्मिक कट्टरवाद
(D) कोई नहीं।
उत्तर:
तार्किकता तथा विज्ञान।
5. हमारा देश ………………… संस्कृति से काफी प्रभावित हुआ है।
(A) उत्तरी
(B) दक्षिणी
(C) पूर्वी
(D) पश्चिमी।
उत्तर:
पश्चिमी।
6. किसने कहा था कि धर्म निष्पक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान तथा समानता?
(A) गाँधी
(B) नेहरू
(C) मौलाना अबुल कलाम
(D) सरदार पटेल।
उत्तर:
गाँधी।
7. भारत में पर्दा प्रथा किसने शुरू की थी?
(A) हिंदुओं ने
(B) मुसलमानों ने
(C) सिक्खों ने
(D) पारसियों ने।
उत्तर:
मुसलमानों ने।
8. 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या मुसलमान है?
(A) 10%
(B) 13%
(C) 14%
(D) 16%
उत्तर:
13%
9. इनमें से कौन-सी किताब एम० एन० श्रीनिवास ने लिखी है?
(A) Cultural change in India
(B) Social change in Modern India
(C) Geographical change in Modern India
(D) Regional change in Modern India.
उत्तर:
Social change in Modern India
10. प्राचीन भारत में कौन-सी धार्मिक भाषा प्रयुक्त होती थी?
(A) पाली
(B) हिंदी
(C) संस्कृत
(D) पंजाबी।
उत्तर:
संस्कृत।
11. उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें निम्न जातियों के लोग उच्च जातियों की नकल करना शुरू कर देते हैं?
(A) पश्चिमीकरण
(B) संस्कृतिकरण
(C) धर्म निष्पक्षता
(D) आधुनिकीकरण।
उत्तर:
संस्कृतिकरण।

12. जब किसी देश का समाज अथवा संस्कृति परिवर्तित होना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं?
(A) सामाजिक परिवर्तन
(B) धार्मिक परिवर्तिन
(C) सांस्कृतिक परिवर्तन
(D) उद्विकासीय परिवर्तन।
उत्तर:
सांस्कृतिक परिवर्तन।
13. प्राचीन समय से आज तक मनुष्य ने जो भी प्राप्त किया है उसे क्या कहते हैं?
(A) सभ्यता
(B) संस्कृति
(C) समाज
(D) चीजों का एकत्र।
उत्तर:
संस्कृति।
14. संस्कृति किस प्रकार का व्यवहार है?
(A) पैतृक
(B) सामाजिक
(C) समाज
(D) कोई नहीं।
उत्तर:
सामाजिक।
15. इस्लाम ने हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है?
(A) हमारे समाज में पर्दा प्रथा आई
(B) जाति व्यवस्था की पाबंदियां अधिक कठोर हो गई
(C) विवाह से संबंधित पाबंदियां और कठोर हो गईं
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
16. धर्म निष्पक्षता को अपनाने का क्या कारण है?
(A) कम होते धार्मिक संस्थान
(B) आधुनिक शिक्षा
(C) पश्चिमी संस्कृति को अपनाना
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
17. धर्म निष्पक्षता ने किस प्रकार हमारे देश के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है?
(A) पवित्रता तथा अपवित्रता के संकल्पों में परिवर्तन
(B) परिवार की संस्था में परिवर्तन।
(C) ग्रामीण समुदाय में बहुत से परिवर्तन आए हैं
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
18. परिवार की संस्था में धर्म निष्पक्षता के कारण किस प्रकार के परिवर्तन आये हैं?
(A) संयुक्त परिवारों का टूटना
(B) एकांकी परिवारों का बढ़ना
(C) परिवार में बड़ों का कम होता नियंत्रण
(D) a + b + c.
उत्तर:
a + b + c
19. धर्म निष्पक्षता के कारण ग्रामीण समुदाय में किस प्रकार का परिवर्तन आया है?
(A) चुनी हुई पंचायतों का सामने आना
(B) समृद्धि पर आधारित सम्मान
(C) अंतर्जातीय विवाहों का बढ़ना
(D) a + b + c
उत्तर:
a + b + c
20. भारत में इस्लाम का प्रभाव पड़ना कब शुरू हुआ?
(A) 13वीं शताब्दी
(B) 14वीं शताब्दी
(C) 15वीं शताब्दी
(D) 16वीं शताब्दी।
उत्तर:
13वीं शताब्दी।
21. The Caste Disability Prohibition Act कब पास हुआ था?
(A) 1842
(B) 1846
(C) 1850
(D) 1854
उत्तर:
1850
22. इनमें से कौन-सा धर्म निष्पक्षता का कारण है?
(A) नगरीकरण
(B) यातायात तथा संचार के साधन
(C) आधुनिकी शिक्षा
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
23. इनमें से कौन-सा अधिकार नागरिकों को भारतीय संविधान ने दिया है?
(A) संपत्ति का अधिकार
(B) साधारण अधिकार
(C) मौलिक अधिकार
(D) कोई नहीं।
उत्तर:
मौलिक अधिकार।
24. पश्चिमीकरण का सिद्धांत किसने दिया था?
(A) श्रीनिवास
(B) मजूमदार
(C) घुर्ये
(D) मुखर्जी।
उत्तर:
श्रीनिवास।
25. पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) जाति प्रथा कमजोर हो गई
(B) तलाक बढ़ गए
(C) केंद्रीय परिवार सामने आए
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
26. इनमें से कौन-सा पश्चिमीकरण का परिणाम है?
(A) संस्थाओं में परिवर्तन
(B) शिक्षा का फैलना
(C) मूल्यों में परिवर्तन
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
27. इनमें से कौन-सी संस्कृतिकरण की विशेषता है?
(A) स्थिति परिवर्तन
(B) उच्च जातियों की नकल
(C) कई माडल
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।

28. संस्कृतिकरण का निम्न जातियों पर क्या प्रभाव पड़ा?
(A) निम्न जातियों में गतिशीलता
(B) निम्न जातियों की स्थिति में सुधार
(C) निम्न जातियों के पेशे में परिवर्तन
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
29. इनमें से कौन-सा देश भारत में पश्चिमीकरण का माडल है?
(A) ब्रिटेन
(B) अमेरिका
(C) जर्मनी
(D) फ्रांस।
उत्तर:
ब्रिटेन।
30. इनमें से कौन-सा पश्चिमीकरण का लक्षण है?
(A) आधुनिकीकरण से अलग
(B) भारतीय समाज पर ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव
(C) केवल शहरियों तक ही सीमित नहीं
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
31. आधुनिकीकरण का मुख्य आधार क्या है?
(A) अच्छाई
(B) बुराई
(C) अच्छाई तथा बुराई
(D) कोई नहीं।
उत्तर:
अच्छाई तथा बुराई।
32. कोई चीज़ जो पहले से नईं तथा अच्छी हो उसे क्या कहते हैं?
(A) आधुनिक
(B) औद्योगिक
(C) प्राचीन
(D) नगरीय।
उत्तर:
आधुनिक।
33. धर्म-निष्पक्षता, शिक्षा, नगरीकरण, नए अधिकार, मशीनें इत्यादि ……………. के लिए आवश्यक है।
(A) औद्योगिकरण
(B) आधुनिकीकरण
(C) संस्कृतिकरण
(D) नगरीकरण।
उत्तर:
आधुनिकीकरण।
34. भारत में कौन-सा उद्योग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है?
(A) कपड़ा उद्योग
(B) लोहा उद्योग
(C) चीनी उद्योग
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
35. भारत में आधुनिकीकरण लाने के लिए कौन उत्तरदायी है?
(A) मुगल शासक
(B) भारत सरकार
(C) ब्रिटिश सरकार
(D) कोई नहीं।
उत्तर:
ब्रिटिश सरकार।
36. उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो परिवर्तन पर आधारित है तथा जो किसी चीज़ की अच्छाई तथा बुराई के बारे में बताती है?
(A) संस्कृतिकरण
(B) औद्योगीकरण
(C) नगरीकरण
(D) आधुनिकीकरण।
उत्तर:
आधुनिकीकरण।
37. उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें निम्न जातियाँ उच्च जातियों में मिल जाती हैं?
(A संस्कृतिकरण
(B) नगरीकरण
(C) औद्योगीकरण
(D) आधुनिकीकरण।
उत्तर:
संस्कृतिकरण।
38. आधुनिकीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
(A) शिक्षा का उच्च स्तर
(B) यातायात तथा संचार के साधनों में विकास
(C) उद्योगों को प्राथमिकता देना
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
39. 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में किन कुरीतियों को रोकने के लिए विशेष बल दिया गया?
(A) सती प्रथा
(B) बाल विवाह
(C) विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
40. इनमें से कौन-सी संकल्पना श्री एम. एन. श्रीनिवास की देन है?
(A) संस्कृतिकरण
(B) पश्चिमीकरण
(C) प्रबल जाति
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर:
उपर्युक्त सभी।
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
संस्कृतिकरण की अवधारणा किस ने दी है?
उत्तर:
संस्कृतिकरण की अवधारणा एम० एन० श्रीनिवास ने दी है।
प्रश्न 2.
पश्चिमीकरण की अवधारणा किस ने दी है?
उत्तर:
पश्चिमीकरण की अवधारणा एम० एन० श्रीनिवास ने दी है।
प्रश्न 3.
भारत किस प्रकार का राज्य है?
उत्तर:
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा धर्म-निरपेक्षता उसे संविधान ने दी है।
प्रश्न 4.
धर्म-निरपेक्ष देश किसे कहते हैं?
उत्तर:
धर्म-निरपेक्ष देश वह होता है जहां किसी एक खास धर्म का आदर न होकर बल्कि सभी धर्मों का आदर हो तथा देश का अपना कोई धर्म न हो। सारे धर्म उसके लिए बराबर हों।
प्रश्न 5.
धर्म-निरपेक्षता का ज़रूरी तत्त्व क्या है?
उत्तर:
धार्मिक कट्टरता (संकीर्णता) का खात्मा धर्म-निरपेक्षता का ज़रूरी तत्त्व होता है।
प्रश्न 6.
धर्म-निरपेक्षता से किस जाति का प्रभाव कम हुआ है?
उत्तर:
धर्म-निरपेक्षता से ब्राह्मण जाति का प्रभाव कम हुआ है क्योंकि अब सभी धर्म तथा जातियां बराबर हैं।
प्रश्न 7.
धर्म-निरपेक्षता का मुख्य आधार क्या होता है?
उत्तर:
विज्ञान तथा तार्किकता धर्म-निरपेक्षता का मुख्य आधार होता है।
प्रश्न 8.
कहां की संस्कृति ने हमारे देश को प्रभावित किया है?
उत्तर:
पश्चिम की संस्कृति ने हमारे देश को प्रभावित किया है।
प्रश्न 9.
गांधी जी के अनुसार धर्म-निरपेक्ष क्या होता है?
उत्तर:
गांधी जी के अनुसार सभी धर्मों का आदर तथा बराबरी धर्म-निरपेक्ष का अर्थ होता है।
प्रश्न 10.
भारत में पर्दा प्रथा किसने शुरू की थी?
उत्तर:
भारत में पर्दा प्रथा मुसलमानों ने शुरू की थी।
प्रश्न 11.
भारत में कितने मुस्लिम रहते हैं?
उत्तर:
भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 13% मुसलमान रहते हैं।
प्रश्न 12.
संस्कृतिकरण के दो सहायक कारक बताओ।
उत्तर:
औद्योगीकरण तथा नगरवाद संस्कृतिकरण के दो सहायक कारक हैं।
प्रश्न 13.
श्रीनिवास ने किस किताब में संस्कृतिकरण की व्याख्या की है?
अथवा
आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक किस विचारक से संबंधित है?
उत्तर:
श्रीनिवास ने किताब लिखी थी Social Change in Modern India जिस में उन्होंने संस्कृतिकरण की व्याख्या की है।

प्रश्न 14.
आधुनिकीकरण के मुख्य आधार क्या होते हैं?
उत्तर:
आधुनिकीकरण के मुख्य आधार अच्छाई और बुराई होते हैं।
प्रश्न 15.
कौन-सी चीज़ आधुनिक होती है?
उत्तर:
जो चीज़ पुरानी चीज़ की जगह नयी तथा अच्छी हो उस चीज़ को आधुनिक कहते हैं।
प्रश्न 16.
आधुनिकीकरण के लिए क्या ज़रूरी है?
उत्तर:
धर्म निरपेक्षता, शिक्षा, नगरीयकरण, नयी मशीनें, नए आविष्कार आधुनिकीकरण के लिए जरूरी हैं।
प्रश्न 17.
भारत में आधुनिकीकरण कब शुरू हुआ था?
उत्तर:
भारत में आधुनिकीकरण अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुआ जब उन्होंने यहां पर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार तथा नयी फैक्टरियां लगानी शुरू की।
प्रश्न 18.
भारत में आधुनिकीकरण से प्रभावित तीन उद्योगों के नाम बताएं।
उत्तर:
- कपड़ा उद्योग
- लोहा उद्योग
- चीनी उद्योग।
प्रश्न 19.
संस्कृतिकरण से किस में परिवर्तन होता है?
उत्तर:
संस्कृतिकरण से जाति व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है जब छोटी जाति के लोग बड़ी जाति में मिलने की कोशिश करते हैं।
प्रश्न 20.
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
उत्तर:
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी।
प्रश्न 21.
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
अथवा
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई?
उत्तर:
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1820 में की।
प्रश्न 22.
सत्य शोधक समाज किसने चलाया था?
उत्तर:
सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के खिलाफ चलाया था।
प्रश्न 23.
ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल कहाँ खोला था?
उत्तर:
ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल पूना में खोला था।
प्रश्न 24.
किसने लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला था?
उत्तर:
1851 में ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला था।
प्रश्न 25.
D.A.V. का पूरा नाम क्या है?
उत्तर:
D.A.V. का पूरा नाम दयानंद ऐंग्लो वैदिक है।
प्रश्न 26.
जनजातीय आंदोलन क्यों शुरू हुए थे?
उत्तर:
जनजातीय आंदोलन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शुरू हुए थे ताकि वह औरों की संस्कृति में न मिल जाएं।
प्रश्न 27.
आधुनिक भारत का पिता (Father of Modern India) किसे कहा जाता है?
उत्तर:
राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता (Father of Modern India) कहा जाता है।
प्रश्न 28.
समाज सुधार क्या होता है?
उत्तर:
जब समाज में चल रही कुरीतियों के विरुद्ध समाज के समझदार व्यक्ति कोई आंदोलन करें तथा उन कुरीतियों को बदलने का प्रयास करें तो उसे समाज सुधार कहते हैं।
प्रश्न 29.
समाज सुधार में गतिशीलता क्यों होती है?
उत्तर:
समाज सुधार में गतिशीलता इसलिए होती है क्योंकि समाज सुधार सभी समाजों तथा सभी युगों में एक समान नहीं होता। इसलिए यह गतिशील है।
प्रश्न 30.
समाज कल्याण क्या होता है?
उत्तर:
समाज कल्याण में उन संगठित सामाजिक कोशिशों या प्रयासों को शामिल किया जाता है जिनकी मदद से समाज के सारे सदस्यों को अपने आप को ठीक तरीके से विकसित करने की सुविधाएं मिलती हैं। समाज कल्याण के कार्यों में निम्न तथा पिछड़े वर्गों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि समाज का हर तरफ से विकास तथा कल्याण हो सके।
प्रश्न 31.
समाज कल्याण के क्या उद्देश्य होते हैं?
उत्तर:
- पहला उद्देश्य यह है कि समाज के सदस्यों के हितों की पूर्ति उनकी ज़रूरतों के अनुसार होती रहे।
- ऐसे सामाजिक संबंध स्थापित करना जिससे लोग अपनी शक्तियों का पूरी तरह विकास कर सकें।
प्रश्न 32.
भारत के आज़ादी के आंदोलन से हमें क्या मिला?
उत्तर:
भारत के आजादी के आंदोलन से हमें आजादी मिली। इस आंदोलन में भारत की सारी जनता बगैर किसी भेदभाव के एक-दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी जिस वजह से उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। निम्न जातियों में भी चेतना आई तथा वह उच्च जातियों के समान खड़े हो गए।
प्रश्न 33.
किन्हीं तीन समाज सुधारकों के नाम बताओ।
उत्तर:
- राजा राममोहन राय
- सर सैयद अहमद खान
- स्वामी दयानंद सरस्वती
- स्वामी विवेकानंद।
प्रश्न 34.
बेसिक शिक्षा की धारणा किसने दी थी?
उत्तर:
बेसिक शिक्षा की धारणा महात्मा गांधी ने 1937 में दी थी।
प्रश्न 35.
समाज कल्याण तथा समाज सुधार में कोई मुख्य फर्क बताओ।
उत्तर:
समाज कल्याण तथा समाज सुधार में मुख्य फर्क यह है कि समाज कल्याण में समाज की निम्न जातियों, पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाते हैं जबकि समाज सुधार में समाज में फैली हुई कुरीतियों को दर कर उनमें बदलाव लाने के प्रयास किए जाते हैं।
प्रश्न 36.
स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
उत्तर:
- भारत की विरासत को महत्त्व देना तथा उसे स्पष्ट करना।
- देश के रचनात्मक निर्माण के प्रयास करने।
प्रश्न 37.
रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य।
उत्तर:
- आत्मत्याग करने वाले साधु-संतों को बाहर भेजना ताकि वे वेदों का प्रचार कर सकें।
- मानवीयता के लिए बगैर किसी जात-पात, धर्म, रंग, स्थान के भेदभाव के कार्य करना।
प्रश्न 38.
थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
उत्तर:
- हिंदू धर्म में पुनः चेतना जगाना ताकि सोए हुए हिंदू जाग सकें।
- विश्व भ्रातरी भाव का तथा विश्व के सभी धर्मों की एकता का प्रचार करना।
प्रश्न 39.
सत्यशोधक समाज के क्या उद्देश्य थे?
उत्तर:
- उस समय समाज में चली आ रही ब्राह्मणों की उच्चता या श्रेष्ठता को चुनौती देना।
- शिक्षा, समानता, स्त्रियों की आजादी के प्रयास करने।
प्रश्न 40.
आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य।
उत्तर:
- आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य गुरुकुल प्रथा पर आधारित हिंदुओं की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को दोबारा – जीवित करना।
वेदों के प्रचार पर ज़ोर देना। - उच्च स्तर पर अंग्रेज़ी शिक्षा को महत्त्व देना।
प्रश्न 41.
राजनीतिक आंदोलन क्या होता है?
उत्तर:
जो आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलाए जाएं उन्हें राजनीतिक आंदोलन कहते हैं। जैसे भारत की आज़ादी का आंदोलन।
प्रश्न 42.
सांस्कृतिक आंदोलन क्या होता है?
उत्तर:
जो आंदोलन अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए चलाया जाए उसे सांस्कृतिक आंदोलन कहते हैं। जैसे जनजातीय आंदोलन।
प्रश्न 43.
आज़ादी से पहले जाति आंदोलन क्यों चलाए गए थे?
उत्तर:
- आज़ादी से पहले जाति आंदोलन इसलिए चलाए गए थे ताकि ब्राह्मणों की और जातियों के ऊपर श्रेष्ठता का विरोध किया जा सके।
- जाति स्तरीकरण में अपनी जाति की स्थिति को ऊपर उठाया जा सके।
प्रश्न 44.
स्वामी विवेकानंद के जीवन का क्या मकसद था?
उत्तर:
स्वामी विवेकानंद के जीवन का मकसद आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना तथा दैनिक जीवन के बीच की खाई को खत्म करना था।

प्रश्न 45.
आर्य समाज की कोई दो विशेषताएं बताओ।
उत्तर:
- आर्य समाज ने विधवा विवाह का प्रचार तथा बाल विवाह का विरोध किया।
- आर्य समाज ने अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा सभी को वेदों को पढ़ने की स्वतंत्रता पर जोर दिया।
प्रश्न 46.
पारसियों के सुधार आंदोलन के क्या उद्देश्य थे?
उत्तर:
- पारसी स्त्री शिक्षा पर जोर दे रहे थे।
- पारसियों के सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य विवाह संबंधी रूढ़िवादिता को खत्म करना था।
प्रश्न 47.
मद्रास में भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी?
उत्तर:
डॉ० ऐनी बेसेंट तथा श्रीमती काडसिस ने मद्रास में भारतीय संघ की स्थापना की थी।
प्रश्न 48.
भगत आंदोलन क्या होता है?
उत्तर:
भारत में निम्न जातियां उच्च जातियों के विचारों, तौर-तरीकों, व्यवहारों का अनुसरण करती हैं। इस प्रकार की रुचि तथा अनुसरण की प्रक्रिया को भगत आंदोलन कहते हैं।
प्रश्न 49.
सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं?
उत्तर:
असल में सुधार आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था इसलिए इन आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन कहते हैं।
प्रश्न 50.
भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए?
उत्तर:
अंग्रेजों के आने के बाद भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। इस शिक्षा को ग्रहण करते-करते समाज के बहुत से सुलझे हुए लोगों को पता चला कि उनके समाज में जो रीतियां, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि चल रही हैं वह असल में रीतियां नहीं बल्कि कुरीतियां हैं। उन्हें पश्चिमी देशों में जाने तथा वहां के लोगों से बातें करने का मौका मिला जिससे उनकी आँखें खुल गईं तथा अपने समाज में फैली कुरीतियों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सुधार आंदोलन चल पड़े।
प्रश्न 51.
सर्वोदय शब्द किसने दिया था?
उत्तर:
सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। उनके अनुसार सिद्धांतों वाला व्यक्ति और लोगों को जीवित रखने के लिए खुद मर जाता है।
प्रश्न 52.
हमारे समाज में सती प्रथा क्यों प्रचलित थी?
उत्तर:
- हमारे समाज में सती प्रथा इसलिए प्रचलित थी क्योंकि विवाह को जन्मों का संबंध माना जाता था। इसलिए पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी को भी मरना पड़ता था।
- इसके साथ एक और भी भावना थी कि ऐसा करने से भगवान् खुश हो जाएंगे तथा सती को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
प्रश्न 53.
विवेकानंद के प्रचार के मुख्य अंश क्या थे?
उत्तर:
- जीवन ही धर्म है। इसलिए जीवन को धर्म मानकर जीना चाहिए।
- जीव की सेवा करना शिव की सेवा करने के समान है।
- ईश्वर मनुष्य के अंदर ही वास करता है।
- मनुष्यों की सेवा करने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग ज़रूरी है।
प्रश्न 54.
पुराने समय में किस धार्मिक भाषा का प्रयोग होता था?
उत्तर:
पुराने समय में संस्कृत का धार्मिक भाषा के रूप में प्रयोग होता था।
प्रश्न 55.
संस्कृतिकरण क्या है?
उत्तर:
जब निम्न हिंदू जातियों के लोग उच्च हिंदू जातियों की नकल करने लग जाएं तथा अपने आप को उच्च जाति में मिलाने की कोशिश करें तो उस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं।
प्रश्न 56.
सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है?
उत्तर:
जब किसी समाज या देश की संस्कृति में परिवर्तन होने लग जाएं तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं।
प्रश्न 57.
धर्म-निरपेक्षता का अर्थ दीजिए।
अथवा
धर्म-निरपेक्षीकरण से आप क्या समझते हैं?
अथवा
पंथ निरपेक्षीकरण क्या है?
उत्तर:
धर्म-निरपेक्षता को लौकिकीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहले धार्मिक था वह अब धार्मिक नहीं रहा। अब सभी धर्म बराबर हो गए हैं तथा कोई धर्म छोटा-बड़ा नहीं है। धर्म-निरपेक्षता में विचारों परंपराओं, धर्म इत्यादि में विज्ञान या तार्किकता लाने का प्रयास किया जाता है।
प्रश्न 58.
पश्चिमीकरण से आप क्या समझते है?
अथवा
पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है?
उत्तर:
जब हमारे देश में पश्चिम के देशों के विचारों, तौर-तरीकों इत्यादि को अपनाया जाता है तो उसे पश्चिमीकरण कहते हैं।
प्रश्न 59.
असंस्कृतिकरण क्या होता है?
उत्तर:
यह संस्कृतिकरण का बिल्कुल उल्टा है। जब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के कार्य अपना लें तो उसे असंस्कृतिकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी ब्राह्मण का जूतों की दुकान खोलना। यह आजकल ही मुमकिन है।
प्रश्न 60.
संस्कृति क्या होती है?
उत्तर:
जो कुछ भी मनुष्य ने प्राचीन समय से लेकर आज तक अपनी बुद्धिमता से हासिल किया है वह उसकी संस्कृति होती है। यह ऐसे विचारों, भावों, तरीकों का जोड़ है जो एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है।
प्रश्न 61.
पुनः संस्कृतिकरण क्या होता है?
उत्तर:
जब एक निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के हाव-भाव, रहने-सहने के तरीके या संस्कृति अपनाते हैं तो वह संस्कृतिकरण होता है। पर जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति की संस्कृति को छोड़ कर दोबारा अपनी संस्कृति या तौर-तरीकों को अपना लेते हैं तो उसे पुनः संस्कृतिकरण कहते हैं।
प्रश्न 62.
इस्लाम धर्म ने हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाले हैं?
उत्तर:
- इस्लाम धर्म से ही परदा प्रथा हमारे समाज में आई।
- इस्लाम धर्म ने ही हमारी जाति प्रथा पर प्रभाव डाला उसके प्रतिबंध और सख्त हो गए।
- इस्लाम धर्म की वजह से हमारे विवाह संबंधी बंधन और सख्त हो गए।
प्रश्न 63.
संस्कृतिकरण की कोई दो विशेषताएं बताओ।
उत्तर:
- संस्कृतिकरण में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुसरण किया जाता है।
- यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
- इसमें निम्न वर्गों का सामाजिक परिवर्तन हो जाता है।
प्रश्न 64.
पश्चिमीकरण ने हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाले?
अथवा
भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के कोई दो प्रभाव बताइये।
उत्तर:
- पश्चिमीकरण की वजह से जाति प्रथा कमजोर हुई।
- इस की वजह से विवाह संबंध-विच्छेद तथा तलाक बढ़ने लगे।
- इस की वजह से औरतों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया।
प्रश्न 65.
प्रभु जाति क्या होती है?
उत्तर:
वह जाति जिसके पास कृषि योग्य भूमि ज्यादा होती है तथा जिसका निम्न जातियां अनुसरण करती हैं वह प्रभु जाति होती है।
प्रश्न 66.
आधुनिकीकरण किसे कहते हैं?
अथवा
आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है?
अथवा
आधुनिकीकरण क्या है?
अथवा
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं?
उत्तर:
वह प्रक्रिया जो परिवर्तन की प्रक्रिया पर आधारित होती है तथा जिसमें अच्छे बुरे, नई पुरानी इत्यादि भावनाओं का आभास होता है, वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होती है। धर्म निरपेक्षता, शिक्षा, नगरीकरण, नई मशीनें, नए अधिकार इत्यादि आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है।
प्रश्न 67.
आधुनिकीकरण के तीन नकारात्मक प्रभाव बताएं।
उत्तर:
- आधुनिकीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तथा केंद्रीय परिवार सामने आ रहे हैं।
- भोग विलास की चीजें बढ़ रही हैं जिसका नई पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
- इस कारण लोगों में अनैतिकता बढ़ रही है तथा समाज में अनैतिक कार्य बढ़ रहे हैं।
प्रश्न 68.
आधुनिकीकरण को संभव बनाने के लिए कौन-सी प्रमुख परिस्थितियाँ आवश्यक हैं?
उत्तर:
आधुनिकीकरण को संभव बनाने के लिए सरकार की दृढ़ शक्ति, जनता की राय, उच्च शिक्षा का होना, धन की बहुतायत, उद्योगों का होना इत्यादि अति आवश्यक है।
प्रश्न 69.
आधुनिकता की परिभाषा एस० सी० दूबे के अनुसार बताएं।
उत्तर:
दूबे के अनुसार, “आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं तथा सामाजिक आदर्श नियमों की ओर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है।
प्रश्न 70.
आधुनिकीकरण के लिए क्या ज़रूरी है?
अथवा
आधुनिकीकरण को संभव बनाने के लिए कौन-सी प्रमुख परिस्थितियां आवश्यक हैं?
उत्तर:
- इसके लिए शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए।
- यातायात तथा संचार के साधनों का विकास होना चाहिए।
- संचार के माध्यमों का भी विकास होना चाहिए।
- कृषि की जगह उद्योग ज्यादा होने चाहिएं।
प्रश्न 71.
भारत एक ………………. देश है।
उत्तर:
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
प्रश्न 72.
संस्कृति के मूर्त भाग को ……………….. कहते हैं।
उत्तर:
संस्कृति के मूर्त भाग को भौतिक संस्कृति कहते हैं।
प्रश्न 73.
शिक्षा की परिभाषा दें।
उत्तर:
ब्राउन तथा रासेक के अनुसार, “शिक्षा अनुभव की वह संपूर्णता है जो किशोर और वयस्क दोनों की अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है तथा उनके व्यवहारों का निर्धारण करती है।”
प्रश्न 74.
शिक्षा के दो कार्य लिखें।
उत्तर:
- शिक्षा व्यक्ति को घटनाओं का सही विश्लेषण करने का ज्ञान देकर उसे समाज का अंग बना देती है।
- शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य समाज में से अनैतिकता, हिंसा, संघर्ष, स्वार्थ इत्यादि बुराइयों को दूर करना तथा इसके स्थान पर नैतिकता, प्यार इत्यादि का विकास करना है।
प्रश्न 75.
औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं?
उत्तर:
औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हम औपचारिक तौर पर स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय इत्यादि में जाकर प्राप्त करते हैं। इस तरह की शिक्षा में स्पष्ट पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है तथा उसके अनुसार ही शिक्षा दी जाती है।
प्रश्न 76.
अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं?
उत्तर:
अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति स्कूल, कॉलेज में नहीं बल्कि अपने रोजाना के अनुभव, अन्य व्यक्तियों के विचारों, परिवार, पड़ोस इत्यादि से प्राप्त करता है। व्यक्ति जो कुछ भी अपने रोज़ाना जीवन से सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं।
प्रश्न 77.
संस्कृति किसे कहते हैं?
उत्तर:
आदिकाल से लेकर आज तक जो कुछ मनुष्य ने प्राप्त किया है वह उसकी संस्कृति है। विचार, फिलासफी, भावनाएं, मशीनें, कारें, बसें, शिक्षा इत्यादि सब कुछ संस्कृति का हिस्सा है।
प्रश्न 78.
सभ्यता किसे कहते हैं?
उत्तर:
संस्कृति के विकसित रूप को सभ्यता कहते हैं अर्थात् जब संस्कृति विकसित हो जाती है तो सभ्यता की स्थिति सामने आती है।
प्रश्न 79.
ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य।
उत्तर:
ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा विवाह की मनाही इत्यादि को दूर करता था।
प्रश्न 80.
वेद ………………….. का धार्मिक ग्रंथ है।
अथवा
वेद किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं?
उत्तर:
वेद हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है।
प्रश्न 81.
कुरान ………………….. का धार्मिक ग्रंथ है।
उत्तर:
करान मसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है।
प्रश्न 82.
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
उत्तर:
आर्य समाज में संस्थापक दयानंद सरस्वती थे।
प्रश्न 83.
संस्कृतिकरण का प्रभुजाति मॉडल क्या है?
उत्तर:
ब्राह्मण संस्कृतिकरण का प्रभुजाति मॉडल है।
प्रश्न 84.
बाइबल …………………. का धार्मिक ग्रंथ है।
उत्तर:
बाइबल इसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है।
प्रश्न 85.
संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
उत्तर:
संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एम० एन० श्रीनिवास ने किया था।
प्रश्न 86.
संस्कृतिकरण का वर्ण मॉडल क्या है?
उत्तर:
संस्कृतिकरण का वर्ण मॉडल ब्राह्मण वर्ण है।
प्रश्न 87.
‘गुरुग्रंथ साहिब’ किस धर्म के अनुयायियों की धार्मिक पुस्तक है?
उत्तर:
‘गुरुग्रंथ साहिब’ सिक्ख धर्म के अनुयायियों की धार्मिक पुस्तक है।
प्रश्न 88.
संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रो० एम० एन० श्रीनिवासन ने दी है। यह कथन सही है या गलत।
उत्तर:
यह कथन सही है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रो० एम० एन० श्रीनिवासन ने दी है।
प्रश्न 89.
भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है या नहीं?
उत्तर:
भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है।
प्रश्न 90.
स्वामी दयानंद सरस्वती ने ‘आर्य समाज’ की स्थापना की या ‘ब्रह्म समाज’ की?
उत्तर:
स्वामी दयानंद सरस्वती ने ‘आर्य समाज’ की स्थापना की।
प्रश्न 91.
भारत पर पश्चिमीकरण के अंतर्गत किस देश का प्रभाव पड़ा?
उत्तर:
भारत पर पश्चिमीकरण के अंतर्गत इंग्लैंड का प्रभाव पड़ा।
प्रश्न 92.
भारत के किसी प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक का नाम बताएँ।
उत्तर:
मुस्लिम समुदाय भारत का प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है।
प्रश्न 93.
भारत में उपनिवेशवाद का अंत कब हुआ?
उत्तर:
भारत में उपनिवेशवाद का अंत 15 अगस्त, 1947 को हुआ जब भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
प्रश्न 94.
गीता किस धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है?
उत्तर:
गीता हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है।

प्रश्न 95.
संस्कृतिकरण का संबंध किसमें परिवर्तन होने से है?
उत्तर:
संस्कृतिकरण का संबंध जाति में परिवर्तन होने से है।
प्रश्न 96.
भारत सरकार किस धर्म को मान्यता प्रदान करती है?
उत्तर:
भारत सरकार किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान करती है।
प्रश्न 97.
पश्चिमीकरण का संबंध किससे है?
उत्तर:
पश्चिमीकरण का संबंध पश्चिमी देशों की संस्कृति अपनाने से है।
प्रश्न 98.
राजा राममोहन राय को किस व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है?
उत्तर:
राजा राममोहन राय को भारतीय परिवर्तन के जनक या पितामह के रूप में जाना जाता है।
लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
समाज सुधार आंदोलनों की मदद से हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं?
उत्तर:
भारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें हर किसी को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। पर कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता के जीवन को सुखमय बनाना है। पर यह तभी संभव है अगर समाज में फैली हुई कुरीतियों तथा अंध-विश्वासों को दूर कर दिया जाए। इन को दूर सिर्फ समाज सुधारक आंदोलन ही कर सकते हैं। सिर्फ कानून बनाकर कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए समाज में सुधार ज़रूरी हैं। कानून बना देने से सिर्फ कुछ नहीं होगा।
उदाहरण के तौर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बच्चों से काम न करवाना। इन सभी के लिए कानून हैं पर ये सब चीजें आम हैं। दहेज लिया दिया, यहां तक कि मांग कर लिया जाता है, बाल विवाह होते हैं, विधवा विवाह को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हमारे समाज के विकास में यह चीजें सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अगर हमें समाज का विकास करना है तो हमें समाज सुधार आंदोलनों की आवश्यकता है। इसलिए हम समाज सुधार आंदोलनों के महत्त्व को भूल नहीं सकते।
प्रश्न 2.
सामाजिक आंदोलन की कोई चार विशेषताएं बताओ।
उत्तर:
- सामाजिक आंदोलन हमेशा समाज विरोधी होते हैं।
- सामाजिक आंदोलन हमेशा नियोजित तथा जानबूझ कर किया गया प्रयत्न है।
- इसका उद्देश्य समाज में सुधार करना होता है।
- इसमें सामूहिक प्रयत्नों की ज़रूरत होती है क्योंकि एक व्यक्ति समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता।
प्रश्न 3.
सामाजिक आंदोलन की किस प्रकार की प्रकृति होती है?
उत्तर:
- सामाजिक आंदोलन संस्थाएं नहीं होते हैं क्योंकि संस्थाएं स्थिर तथा रूढ़िवादी होती हैं तथा संस्कृति का ज़रूरी पक्ष मानी जाती हैं। यह आंदोलन अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद खत्म हो जाते हैं। सामाजिक आंदोलन समितियां भी नहीं हैं क्योंकि समितियों का
- एक विधान होता है। यह आंदोलन तो अनौपचारिक, असंगठित तथा परंपरा के विरुद्ध होता है।
- सामाजिक आंदोलन दबाव या स्वार्थ समूह भी नहीं होते बल्कि यह आंदोलन सामाजिक प्रतिमानों में बदलाव की मांग करते हैं।
प्रश्न 4.
ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
उत्तर:
राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-
- इनका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा विवाह की मनाही इत्यादि को दूर करना था।
- यह समाज स्त्रियों को शिक्षा देकर समाज में ऊँचा दर्जा दिलाने के पक्ष में था।
- ब्रह्म समाज अंतर्जातीय विवाहों को भी करवाने के पक्ष में था।
- ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से ही सती प्रथा निरोधक कानून 1829 तथा विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 . बना था।
प्रश्न 5.
19वीं तथा 20वीं शताब्दी के कुछ संगठनों के नाम बताओ जिन्होंने समाज सुधार के कार्य किए थे।
उत्तर:
- आर्य समाज
- ब्रह्म समाज
- प्रार्थना समाज
- संगत सभा
- रामकृष्ण मिशन
- हरिजन सेवक संघ
- विधवा विवाह संघ
- आर्य महिला समाज।
प्रश्न 6.
मुसलमानों में जो सुधार कार्य किए गए उनका वर्णन करो।
उत्तर:
मुसलमानों में सुधार आंदोलन चलाने का श्रेय सर सैय्यद अहमद खान को जाता है। 1857 के पश्चात उन्होंने देखा कि मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी हैं तथा अंग्रेज़ उन पर अत्याचार कर रहे हैं तथा इन्हें दबा रहे हैं। इसलिए मुस्लिमों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने सुधार कार्य शुरू किए। उन्होंने मुस्लिमों में फैली बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसमें मुसलमानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए उत्साहित किया।
उन्हीं की कोशिशों से 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल खोला गया जो 1918 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तबदील हो गया। उन्होंने बहु-पत्नी विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार किया। वह स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। इसी तरह कई और मुस्लिम समाज सुधारकों ने मुस्लिमों में जागृति लाने के प्रयास किए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिनके प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान की स्थापना हुई।
प्रश्न 7.
स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है लोगों के दवारा देश में ही बनी चीज़ों का उपयोग करना, अपने देश की संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना, देसी उद्योगों की स्थापना करना। इस के साथ साथ विदेशी चीजों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, दुकानों आदि का बहिष्कार करना। यह शुरू हुआ था 1905 के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने की नीयत से बंगाल को दो भागों में बांट दिया।
इसके विरोध में लोगों ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया जो कि शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। इसमें स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया तथा विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। आम जनता ने भी इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी चीज़ों की खपत बढ़ गई, भारतीय उद्योगों का विकास हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन मिला तथा सरकार के विरुदध व्यापक जनाधार बन गया।
प्रश्न 8.
जनजातीय आंदोलन क्यों शुरू हुए थे?
उत्तर:
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सैंकड़ों जनजातियों के लोग रहते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट जीवन शैली होती है। उनकी ज़रूरतें भी कम होती हैं। वह अपनी संस्कृति व अलग जनजातीय पहचान बनाए रखने के प्रति बहुत सचेत होते हैं। यदि जनजाति के सदस्यों को लगे कि उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ की जा रही है, इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है या उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है या उनकी अपनी अलग पहचान बनाए रखने में कोई खतरा है तो वे आंदोलन का रास्ता अपना लेते हैं।
इसके अलावा अन्य समदायों, धर्मों तथा वर्गों के लोगों के प्रभाव के कारण निश्चित तरह के परिवर्तन की इच्छा से भी जनजातियों के लोग आंदोलन करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार से झारखंड राज्य अलग करने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ। बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति में ईसाइयत के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बिरसा को मुंडा जनजाति के लोग बिरसा भगवान् कहते थे। उसके कहने के फलस्वरूप इस जनजाति के उन लोगों, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, ने हिंदू धर्म को पुनः अपना लिया तथा मूर्ति पूजा, हिंदू कर्म-कांडों तथा रीति-रिवाजों का पालन करने लगे।
प्रश्न 9.
पारसियों में सुधार आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के अलग-अलग समुदायों तथा वर्गों के लोगों ने सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन चलाए। पारसी भी समाज सुधार आंदोलनों में पीछे नहीं रहे। सन् 1851 में पारसी नेताओं दादा भाई नौरोजी (Dadabhai Naoroji), नौरोजी फुरदोंजी (Naoroji Furdonji) तथा जे० बी० बाचा (J.B. Bacha) इत्यादि ने मिलकर ‘रेहनुमाइ मजदयासन सभा’ या धार्मिक सुधार सभा का गठन किया।
पारसी धर्म में सुधार लाना तथा इस धर्म के सदस्यों को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ जोड़ना इस सभा का प्रमुख उद्देश्य था। 1900 में पारसियों ने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। इन सब गतिविधियों के अलावा पत्रिकाओं व समाचार-पत्रों में लेखों, भाषणों तथा बैठकों के माध्यम से पारसी नेताओं ने पारसी धर्म के अनुयायियों को धार्मिक रूढ़ियों व अंध-विश्वासों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए। इन सब प्रयासों के कारण पारसी आज भारतीय समाज के सबसे पश्चिमीकृत वर्ग बन गए हैं।
प्रश्न 10.
राजा राममोहन राय ने भारत के समाज सुधारों में क्या योगदान दिया था?
अथवा
समाज, धर्म और स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राजा राममोहन राय ने क्या प्रयास किया?
उत्तर:
राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। उन्होंने भारतीय समाज सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया जिसका वर्णन निम्नलिखित है-
- राजा राममोहन राय की कोशिशों के फलस्वरूप भारतीय समाज में चली आ रही बहुत बड़ी कुरीति सती प्रथा को 1829 में कानून बनाकर ब्रिटिश सरकार ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया था।
- राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रहमो समाज की स्थापना की जो काफी समय तक भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने में लगा रहा।
- राजा राममोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने खुद भी पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की थी तथा उन्होंने युवाओं को भी पश्चिमी शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया।
- उन्होंने जाति प्रथा, जो कि भारतीय समाज को काफ़ी हद तक खोखला कर चुकी थी, के विरुद्ध भी जमकर आवाज़ उठाई।
- उन्होंने स्त्रियों को ऊपर उठाने के काफी प्रयास किए। वह सती प्रथा, बाल विवाह के विरोधी तथा विधवा विवाह और स्त्रियों की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे।
प्रश्न 11.
रामकृष्ण मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
उत्तर:
रामकृष्ण मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-
- सभी जातियों व संप्रदायों के लोगों को दयायुक्त, दानयुक्त तथा मानवीय कार्य करवाना।
- सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को खत्म करना।
- स्त्रियों का स्थान उच्च करने के लिए कार्य करना।
- सब जीवमात्र की सेवा का प्रचार करना।
- मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना।
- आत्मत्यागी तथा व्यावहारिक अध्यात्मवादी साधुओं को रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के प्रचार तथा प्रसार के लिए तैयार करना।
प्रश्न 12.
भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए?
उत्तर:
भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित कारणों से शुरू हुए-
- भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को धर्म के साथ जोड़ा हुआ था।
- समाज का जातीय आधार पर विभाजन था तथा जाति धर्म के आधार पर बनी हुई थी। जाति के नियमों को तोड़ना पाप माना जाता था।
- भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी निम्न थी जिस वजह से उनका कोई महत्त्व नहीं रह गया था।
- भारतीय समाज में अशिक्षा का बोलबाला था।
- जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह की मनाही इत्यादि बहुत-सी कुरीतियां समाज में फैली हुई थीं।
इन सब कारणों की वजह से शिक्षित समाज सुधारकों ने समाज सुधार करने की ठानी तथा समाज सुधार आंदोलन शुरू हो गए।
प्रश्न 13.
समाज में फैली कुरीतियों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे?
उत्तर:
समाज में फैली बहुत-सी बुराइयों या कुरीतियों पर गांधी जी के निम्नलिखित विचार थे-
- गांधी जी के अनुसार निम्न जातियों को उच्च जातियों के बराबर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने निम्न जातियों के लोगों को हरिजन का नाम दिया तथा उनके उत्थान के कई कार्य किए।
- स्त्रियां भी उनके अनुसार पुरुषों के समान हैं। इसलिए गांधी जी ने स्त्रियों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में आमंत्रित किया जिस वजह से लाखों स्त्रियां इस आंदोलन में कूद पड़ी।
- गांधी जी नशाखोरी के भी विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने 1926 में इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था।
- उनके अनुसार जब तक भारतीय समाज से अस्पृश्यता खत्म नहीं हो जाती तब तक आजादी का कोई फायदा नहीं है।
- गांधी जी दहेज प्रथा के भी विरुद्ध थे। उनके अनुसार दहेज लेने वाले देश के गद्दार हैं।
प्रश्न 14.
आज़ादी से पहले चले सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं क्या थी?
उत्तर:
आज़ादी से पहले चले सामाजिक आंदोलनों की निम्नलिखित विशेषताएं थीं-
- आजादी से पहले चले सामाजिक आंदोलनों की पहली विशेषता यह थी कि हिंदू धर्म को तार्किक रूप से स्थापित करना क्योंकि इसने मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजों के कई थपेड़ों को झेला था।
- महिलाओं, हरिजनों तथा शोषित वर्गों को ऊपर उठाना ताकि यह वर्ग भी और वर्गों की तरह सर उठाकर जी सकें।
- ये आंदोलन परंपरागत रूढ़िवादी विचारधाराओं को समाप्त करके उनकी जगह नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे।
- ये आंदोलन जाति व्यवस्था की असमानता की बेड़ियों को तोड़कर समानता तथा भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहते थे।
- ये आंदोलन भारतीय जनता में प्यार, भाईचारे, सहनशीलता, त्याग आदि भावनाओं का विकास करना चाहते थे।
प्रश्न 15.
क्रांतिकारी आंदोलन की क्या विशेषताएं होती हैं?
उत्तर:
क्रांतिकारी आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं-
- क्रांतिकारी आंदोलन प्रचलित पुरानी व्यवस्था को उखाड़ कर उसकी जगह नयी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं।
- क्रांतिकारी आंदोलन में हिंसात्मक तथा दबाव वाले तरीके अपनाए जाते हैं।
- क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा तभी चलाए जाते हैं जब सामाजिक बुराइयों को दूर करना हो।
- क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा निरंकुश शासन में तथा उसे खत्म करने के लिए चलाए जाते हैं।
- क्रांतिकारी आंदोलनों में हमेशा उग्रता तथा तीव्रता पाई जाती है।
प्रश्न 16.
सुधारवादी आंदोलन की क्या विशेषताएं होती हैं?
उत्तर:
सुधारवादी आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं-
- सुधारवादी आंदोलन प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहता है।
- सुधारवादी आंदोलनों की गति हमेशा धीमी होती है।
- सुधारवादी आंदोलनों में हमेशा शांतिपूर्ण तरीके अपनाए जाते हैं तथा यह समाज में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए चलाए जाते हैं।
- यह आम तौर पर प्रजातांत्रिक देशों में पाया जाता है।
प्रश्न 17.
सिंह सभा आंदोलन के क्या उद्देश्य थे?
उत्तर:
सिंह सभा आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे-
- सिक्ख धर्म में पवित्रता पुनः स्थापित करना।
- सिक्ख धर्म तथा संस्कृति संबंधी साहित्य का विकास करना।
- धर्म परिवर्तित सिक्खों को वापिस सिक्ख धर्म में वापस लाना।
- सिक्खों में प्रचलित अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को दूर करना।
- शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।
- स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार दिलवाना
- सिक्ख धर्म के प्रचार तैयार कर इसके प्रचार के लिए कार्य करना।
प्रश्न 18.
ब्रहम समाज तथा आर्य समाज में अंतर बताओ।
उत्तर:
ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज में अंतर निम्नलिखित हैं-
- आर्य समाज का एक पवित्र ग्रंथ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ है जबकि ब्रह्म समाज का कोई ग्रंथ नहीं है।
- आर्य समाज में वेदों को ही हर चीज़ का मूल माना गया है जबकि ब्रह्म समाज में ऐसा कुछ नहीं है।
- आर्य समाजी स्वदेशी भाषा को पढ़ने पर जोर देते थे पर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई पर जोर देते थे।
- आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया पर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने पर जोर दिया।
- आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती वैदिक संस्कृति अपनाने पर जोर देते थे पर राजा राममोहन राय को पश्चिमी संस्कृति अपनाने में कोई परेशानी नहीं थी।
प्रश्न 19.
पश्चिमीकरण के क्या परिणाम हो सकते हैं?
अथवा
भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का वर्णन करें।
उत्तर:
पश्चिमीकरण के परिणाम निम्नलिखित हैं-
(i) संस्थाओं में परिवर्तन-पश्चिमीकरण की वजह से हमारे समाज में चल रही कई प्रकार की संस्थाओं में बहुत से परिवर्तन आ गए हैं। विवाह, परिवार, जाति प्रथा, धर्म इत्यादि संस्थाओं में जो रूढ़िवादिता पहले देखने को मिलती थी वह अब देखने को नहीं मिलती।
(ii) मूल्यों में परिवर्तन-इस वजह से मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा प्राप्त करके सभी को समानता के अधिकार के बारे में पता चल रहा है। अब हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है परिवार के बारे में वह बाद में सोचता है। अब व्यक्तिवादिता तथा रस्मी संबंध बढ़ रहे हैं।
(iii) अब धर्म का उतना महत्त्व नहीं रह गया है जितना पहले था। पहले हर व्यक्ति धर्म से डरता था, सारे धार्मिक काम किया करता था पर अब व्यक्ति धर्म का प्रयोग सिर्फ उतना ही करता है जितनी ज़रूरत होती है। यह सब पश्चिमीकरण का ही परिणाम है।
(iv) पश्चिमीकरण की वजह में हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। आज हमारे देश की साक्षरता दर 65% से ऊपर है तथा यह आगे भी बढ़ेगी। इसके साथ ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त होने लग गई है तथा उनकी आजादी बढ़ गई है।
प्रश्न 20.
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में बताएं।
अथवा
संस्कृतिकरण की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
उत्तर:
प्रो० एम० एन० श्रीनिवास के अनुसार, “संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्म-कांड, विचारधारा तथा जीवन शैली को उच्च समूह की दिशा में बदल लेता है। साधारणतया ऐसे परिवर्तनों के बाद वह जाति स्थानीय समुदाय द्वारा जातीय सोपान में उच्च स्थान का दावा करने लगती है। आम तौर पर ऐसा दावा करने के एक-दो पीढ़ियों के बाद उसे स्वीकृति मिल जाती है।
कभी-कभी कोई जाति ऐसे स्थान का दावा करती है जिसे मानने के लिए पड़ोसी जाति सहमत नहीं होती है।” इस तरह संस्कृतिकरण निम्न जाति या समूह की परंपराओं, कर्म-कांडों, विचारधारा तथा जीवन शैली में उच्च जाति की दिशा में परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ऐसे परिवर्तनों के कुछ समय के बाद उक्त समूह जातीय संस्तरण में प्राप्त पारंपरिक स्थान से उच्च स्थान प्राप्ति का दावा करते हैं।
प्रश्न 21.
पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का अर्थ समझाएं।
अथवा
पश्चिमीकरण क्या है?
अथवा
पश्चिमीकरण पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।
उत्तर:
साधारणतया पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों के भारत पर प्रभाव से लिया जाता है। पश्चिमी देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिका ऐसे राष्ट्र हैं जिनका भारतीय समाज पर काफ़ी प्रभाव रहा है। एम० एन० श्रीनिवास ने इसी पश्चिमीकरण की व्याख्या की है। उनके अनुसार, “पश्चिमीकरण शब्द को मैंने ब्रिटिश के 150 से अधिक वर्ष के शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है और यह शब्द विभिन्न स्वरों-प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधाराओं तथा मूल्यों आदि में परिवर्तनों से संबंधित है।”
प्रश्न 22.
धर्म-निरपेक्षता का क्या अर्थ है?
अथवा
धर्म-निरपेक्षतावाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
उत्तर:
भारतीय समाज 20वीं शताब्दी से ही पवित्र समाज से एक धर्म निरपेक्ष समाज में परिवर्तित हो रहा है। इस शताब्दी के अनेक विद्वानों ने यह महसूस किया कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर ही विभिन्न धर्मों का देश भारत संगठित रह पाया है। धर्म-निरपेक्षता के आधार पर राज्य के सभी धार्मिक समूहों एवं धार्मिक विश्वासों को एक समान माना जाता है।
निरपेक्षता का अर्थ समानता या तटस्थता से है। राज्य सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखता है तथा किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्म निरपेक्षता ऐसी नीति या सिद्धांत है जिसके अंतर्गत लोगों को किसी विशेष धर्म को मानने या पालन के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
प्रश्न 23.
संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में भेद बताएं।
उत्तर:
| संस्कृतिकरण | पशिचमीकरण |
| (i) संस्कृतिकरण में कई प्रकार की चीज़ें खाने-पीने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। | (i) पश्चिमीकरण में किसी चीज़ के खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। |
| (ii) यह एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है। | (ii) यह एक तार्किक प्रक्रिया है। |
| (iii) संस्कृतिकरण की प्रक्रिया स्वदेशी तथा आंतरिक है। | (iii) पश्चिमीकरण की प्रक्रिया विदेशी तथा बाहरी है। |
| (iv) संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बहुत पुराने समय से चली आ रही है। | (iv) पशिचमीकरण की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के भारत आने के काफ़ी देर बाद शुरू हुई है। |
| (v) संस्कृतिकरण करने वाली जाति गतिशीलता करके उच्च स्थिति पर पहुंच जाती है। | (v) पश्चिमीकरण में जाति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। |
| (vi) संस्कृतिकरण की प्रक्रिया समाज की कुछ निम्न जातियों तक ही सीमित होती है। | (vi) पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में सभी जातियां समान रूप से हिस्सा लेती हैं। |
प्रश्न 24.
आप पश्चिमी, आधुनिक, पंथनिरपेक्ष तथा सांस्कृतिक प्रकार के व्यवहार को किस रूप में परिभाषित करेंगे क्या आप इन शब्दों के सामान्य अर्थ एवं समाजशास्त्रीय अर्थ में कोई अंतर पाते हैं?
उत्तर:
जब कोई पश्चिम के देशों के विचारों, तौर-तरीकों इत्यादि को अपनाता है तो उसे पश्चिमी कहा जाता है। इस तरह पश्चिमी देशों के प्रभाव को पश्चिमी कहते हैं। आधुनिक वह होता है जिसमें परिवर्तन आ रहा होता है तथा जिसमें अच्छे बुरे, नये पुराने का आभास होता है जो व्यक्ति पश्चिमी देशों की संस्कृति के प्रभाव में आकर कार्य करता है तथा जो प्राचीन परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं को अपनाता है उसे आधुनिक कहते हैं।
पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो पहले धार्मिक था वह अब धार्मिक नहीं रहा। अब सभी धर्म बराबर हो गए हैं तथा कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। धर्म-निरपेक्षता में विचारों, परंपराओं, धर्म इत्यादि में विज्ञान या तार्किकता लाने का प्रयास किया जाता है। पंथनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में धर्म का प्रभाव कम हो जाता है तथा । धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। इस तरह ही सांस्कृतिक शब्द का अर्थ जीवन के स्वीकृत ढंगों में होने वाले परिवर्तन से है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो।
अगर हम ध्यान से देखें तो इन शब्दों के समाजशास्त्रीय अर्थ तथा सामान्य अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि यह संकल्प समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं तथा उन्होंने इनकी व्याख्या जीवन की साधारण दशाओं के अनुसार ही की है।
प्रश्न 25.
आधुनिकता तथा परंपरा के मिश्रण के कुछ उदाहरणों के बारे में बताएं जो आप दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में और व्यापक स्तर पर पाते हैं।
उत्तर:
संस्कृति के दो प्रकार होते हैं-भौतिक तथा अभौतिक। आधुनिकता के साधन भौतिकता के भाग हैं तथा परंपरा अभौतिक संस्कृति का हिस्सा है। हमारे जीवन में आधुनिकता तथा परंपरा के मिश्रण की बहुत-से उदाहरण मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने टी० वी०, फ्रिज बेचने का शोरूम बनाया है, यह आधुनिकता है, परंतु वह अपनी दुकान को बुरी नजर से बचाने के लिए या तो नींबू मिर्चे या फिर हंडिया (नज़रबट्ट) लटका देता है।
यह आधुनिकता तथा परंपरा का मिश्रण है। हम नई कार लेकर आते हैं परंतु घर जाने की बजाए पहले मंदिर जाते हैं ताकि कार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। आमतौर पर ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों इत्यादि के पीछे लिखा होता है ‘बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला’। यह भी आधुनिकता तथा परंपरा के मिश्रण के उदाहरण हैं। हम लोगों ने पश्चिमी समाज के रहन सहन, कपड़े पहनने घर बनाने के ढंग तो अपना लिए हैं, परंतु हमारे विचार अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं जहां पर यह 100 साल पहले थे। यह भी आधुनिकता तथा परंपरा के मिश्रण की उदाहरणें हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के पश्चात् हमने आधुनिकता या फिर कहें कि पश्चिमी समाज के तौर तरीकों, जीवन जीने के ढंगों को अपनाना तो शुरू कर दिया है। परंतु हम अभी भी अपने जाति संबंधी विचारों या धार्मिक विचारों को छोड़ नहीं पाये हैं। हमारे विचार अभी भी प्राचीन समाज में ही अटके पड़े हैं तथा यही कारण है कि आने वाली पीढ़ी तथा जाने वाली पीढ़ी के विचारों में हमेशा ही अंतर रहता है।
प्रश्न 26.
क्या आपको संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में लैंगिक आधार पर सामाजिक भेदभाव के सबूत दिखते हैं?
उत्तर:
अगर हम संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तथा भारतीय समाज की संरचना की तरफ देखें तो हमें लैंगिक आधार पर सामाजिक भेदभाव में बहुत से सबूत मिल जाएँगे। हम उदाहरण ले सकते हैं प्राचीन समाज की जब स्त्रियों को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। उन्हें किसी प्रकार में अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों के साथ-साथ निम्न जातियों के लोगों को भी शोषण से भरपूर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इन लोगों का जीवन नर्क के समान था।
सदियों से इनके साथ ऐसा व्यवहार होता चला आ रहा था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान बना तथा इन सभी शोषित वर्गों तथा अन्य वर्गों को समान अधिकार दिए गए। 1955 के अस्पृश्यता अपराध कानून से निम्न वर्गों की निर्योग्यताएं समाप्त कर दी गई। स्त्रियों की समाज में स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कई प्रकार के विधानों का निर्माण किया गया। इनके कल्याण के कई कार्यक्रम चलाए गए।
इन सब प्रयासों के फलस्वरूप स्त्रियों तथा निम्न जातियों को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए तथा उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ। निम्न जातियों में लोगों ने सामाजिक संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊँचा किया। स्त्रियों ने उच्च शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की तथा उसके बाद वह आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर होना शुरू हो गई।
अगर हम आज के समाज पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिला कर कार्य कर रही हैं। चाहे समाज में लैंगिक आधार पर सामाजिक भेदभाव के सबूत आज भी मिल जाते हैं, परंतु अब यह लैंगिक भेदभाव धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है तथा स्त्रियाँ अपने आपको ऊँचा उठाने के भरसक प्रयास कर रही हैं ताकि यह लैंगिक भेदभाव खत्म हो जाए।
प्रश्न 27.
उन सभी छोटे-बड़े तरीकों का अवलोकन करें जहां पश्चिमीकरण से हमारा जीवन प्रभावित होता है।
अथवा
भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
अगर हम अपने रोजाना के जीवन का अवलोकन करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन का हरेक पक्ष पश्चिमीकरण से प्रभावित हुआ है। हम हरेक पक्ष के बारे में अलग-अलग देख सकते हैं। पहले हम धोती-कुर्ता, कुर्ता पायजामा इत्यादि पहना करते थे, परंतु अब पैंट, शर्ट, कोट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, टाई, ट्रैक सूट इत्यादि पहनते हैं जो कि पश्चिमी देन है। पहले हम नीचे बैठ कर साधारण खाना जैसे कि सब्जी, रोटी, दाल इत्यादि खाते थे परंतु अब हम डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाते हैं।
खाने के प्रकार भी बदल गए हैं। रोटी का स्थान सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, हॉट डाग इत्यादि ने ले लिया है। पहले चाय तथा मदिरा का सेवन होता था, परंतु अब चाय, कॉफी, व्हिसकी, जिन, कोल्ड ड्रिंक, शेक इत्यादि का सेवन होता है। पहले मनोरंजन के साधनों में बड़े बजुर्गों की कहानियाँ होती थीं परंतु अब उनके स्थान पर रेडियो, टेलीविज़न, कम्प्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। गर्मी में फ्रिज का ठंडा पानी तथा ए० सी० प्रयोग होता है और सर्दी में गीज़र का गर्म पानी तथा गर्म हवा वाला ब्लोअर प्रयोग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष पश्चिमीकरण से प्रभावित हुआ है।
प्रश्न 28.
उन दो संस्कृतियों की तुलना करें जिनसे आप परिचित हों। क्या नृजातीय नहीं बनना कठिन नहीं है?
उत्तर:
हम भारतीय सस्कृति तथा पाश्चात्य संस्कृति के वाकिफ हैं। भारतीय संस्कति धर्म से प्रेरित है तथा पाश्चात्य संस्कृति विज्ञान तथा तर्क से प्रेरित है। भारतीय संस्कृति तथा पाश्चात्य संस्कृति एक दूसरे से विपरीत हैं जहां के संस्कार रूढ़ियां, व्यवहार के ढंग, रहन-सहन, खाने-पीने कपड़े पहनने के ढंग एक-दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं।
हम कह सकते हैं कि नृजातीय बनना कठिन है क्योंकि हम दूसरी संस्कृति के भौतिक हिस्से को तो तेजी से अपना लेते हैं परन्तु अभौतिक संस्कृति को अपनाना बहुत मुश्किल होता है जिस कारण हम दूसरी संस्कृति को पूर्णतया अपना नहीं सकते हैं तथा नृजातीय नहीं बन सकते हैं।

प्रश्न 29.
सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए दो विभिन्न उपागमों की चर्चा करें।
उत्तर:
सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक परिवर्तन का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक परिवर्तन किसी भी स्थान की सांस्कृति को पूर्णतया परिवर्तित कर सकते हैं। बाढ़, सूखा, भूकम्प, गर्मी, सर्दी इत्यादि किसी भी स्थान की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही क्रान्तिकारी परिवर्तनों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है।
जब किसी संस्कृति में तेज़ी से परिवर्तन आथा है तो उस संस्कृति के मूल्यों तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आते हैं। क्रान्तिकारी परिवर्तन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही आते हैं जिससे उस समाज की संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए प्राकृतिक परिवर्तनों तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक है।
प्रश्न 30.
आधुनिकीकरण की दो विशेषताएं बताएं।
उत्तर:
1. सामाजिक भिन्नता-आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण समाज के विभिन्न क्षेत्र काफ़ी Complex हो गए तथा व्यक्तिगत प्रगति भी पाई गई। इस वजह से विभेदीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई।
2. सामाजिक गतिशीलता-आधुनिकीकरण के द्वारा प्राचीन सामाजिक, आर्थिक तत्त्वों का रूपांतरण हो जाता है, मनुष्यों के आदर्शों की नई कीमतें स्थापित हो जाती हैं तथा गतिशीलता बढ़ जाती है।
प्रश्न 31.
आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए दो परिवर्तन बताएं।
उत्तर:
1. धर्म-निरपेक्षता-भारतीय समाज में धर्म-निरपेक्षता का आदर्श स्थापित हुआ। किसी भी धार्मिक समूह का सदस्य देश के ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। प्यार, हमदर्दी, सहनशीलता इत्यादि जैसे गुणों का विकास समाज में समानता पैदा करता है। यह सब आधुनिकीकरण के कारण है।
2. औद्योगीकरण-औद्योगीकरण की तेजी के द्वारा भारत की बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतें पूरी करनी काफ़ी आसान हो गईं। एक तरफ बड़े पैमाने के उद्योग शुरू हुए तथा दूसरी तरफ घरेलू उद्योग तथा संयुक्त परिवारों का खात्मा हुआ।
प्रश्न 32.
आधुनिकीकरण तथा सामाजिक गतिशीलता का क्या संबंध है?
उत्तर:
सामाजिक गतिशीलता आधुनिक समाजों की मुख्य विशेषता है। शहरी समाज में कार्य की बांट, विशेषीकरण, कार्यों की भिन्नता, उद्योग, व्यापार, यातायात के साधन तथा संचार के साधनों इत्यादि ने सामाजिक गतिशीलता को काफ़ी तेज़ कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, बुद्धि के साथ गरीब से अमीर बन जाता है।
जिस कार्य से उसे लाभ प्राप्त होता है वह उस कार्य को करना शुरू कर देता है। कार्य के लिए वह स्थान भी परिवर्तित कर लेता है। इस तरह सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के द्वारा परंपरावादी कीमतों की जगह नई कीमतों का विकास हुआ। इस तरह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है।
प्रश्न 33.
आधुनिकीकरण से नए वर्गों की स्थापना होती है। कैसे?
उत्तर:
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को प्रगति करने के कई मौके प्रदान करती है। इस वजह से कई नए वर्गों की स्थापना होती है। समाज में यदि सिर्फ एक ही वर्ग होगा तो वह वर्गहीन समाज कहलाएगा। इसलिए आधुनिक समाज में कई नये वर्ग अस्तित्व में आए हैं।
आधुनिक समाज में सबसे ज्यादा महत्त्व पैसे का होता है। इसलिए लोग जाति के आधार पर नहीं बल्कि राजनीति तथा आर्थिक आधारों पर बंटे हुए होते हैं। वर्गों के आगे आने का कारण यह है कि अलग-अलग व्यक्तियों की योग्यताएं समान नहीं होतीं। मजदूर संघ अपने हितों की प्राप्ति के लिए संघर्ष का रास्ता भी अपना लेते हैं। अलग-अलग कार्यों के लोगों ने तो अलग-अलग अपने संघ बना लिए हैं।
प्रश्न 34.
धर्म-निरपेक्षता में ज़रूरी तत्त्व क्या है?
उत्तर:
- धार्मिक विघटन-धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन पाया गया, व्यावहारिक लाभों को महत्ता प्राप्त हुई। अर्थात् किसी भी धार्मिक क्रिया के बिना आजकल लोगों को प्रभावित किया जा सकता है।
- तार्किकता-प्रत्येक कार्य तथा समस्या के ऊपर तर्क के आधार पर विचार किया जाता है जिससे प्राचीन अन्ध-विश्वासों में कमी हो जाती है।
- विभेदीकरण-समाज के अलग-अलग हिस्से जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा धर्म का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में कम हो गया है।
प्रश्न 35.
धर्म-निरपेक्षता के दो कारण बताएं।
उत्तर:
- आधुनिक शिक्षा-आधुनिक शिक्षा के द्वारा उच्च तथा निम्न की भावना खत्म हुई तथा व्यक्ति को स्थिति भी उसकी योग्यता के आधार पर प्राप्त हुई। लोगों की भावना में भी बढ़ोत्तरी हुई।
- यातायात तथा संचार के साधनों का विकास-यातायात तथा संचार के साधनों के विकास के साथ लोग एक दूसरे के नजदीक आए, अस्पृश्यता, उच्च निम्न के भेदभाव में कमी आई तथा बराबरी वाले संबंध स्थापित हुए।
प्रश्न 36.
धर्म-निरपेक्षता द्वारा लाए गए दो परिवर्तन बताएं।
उत्तर:
- पवित्र तथा अपवित्र के संकल्प में परिवर्तन-प्राचीन समय से चले आ रहे पवित्रता तथा अपवित्रता के विचारों में कमी आयी। हर तरह का तथा प्रत्येक जाति का खाना पवित्र माना गया। सभी धर्मों में बराबरी के संबंध स्थापित हुए।
- संस्कारों में परिवर्तन-हिन्दू धर्म से संबंधित संस्कार जैसे बच्चे के जन्म से सम्बन्धित, विधवा से संबंधित इत्यादि संस्कार खत्म हो गए। व्यक्तिगत योग्यता महत्त्वपूर्ण हो गई।
प्रश्न 37.
धर्म-निरपेक्षता का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर:
भारत में शुरू से ही संयुक्त परिवार प्रणाली प्रमुख रही है क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते थे जिसमें ज्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी। विकास के पक्ष से भी भारत काफ़ी पीछे था। परंतु धर्म-निरपेक्षता के प्रभाव में प्राचीन परंपराओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला। परिवार के कई तरह के कार्य दूसरी संस्थाओं के पास चले गए। संयुक्त परिवार प्रथा बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ गई है।
निबंधात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
सामाजिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन लाए? उनका वर्णन करो।
उत्तर:
भारतीय समाज में 19वीं सदी आते-आते बहुत-सी कुरीतियां फैली हुई थीं। इन कुरीतियों ने भारतीय समाज को बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इसी समय भारत के ऊपर अंग्रेज़ कब्जा कर रहे थे। इसके साथ-साथ वह पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी कर रहे थे। बहुत से अमीर भारतीय पश्चिमी शिक्षा ले रहे थे।
शिक्षा लेने के बाद जब वह भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारतीय समाज बहुत-सी कुरीतियों में जकड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया ताकि इन कुरीतियों को दूर किया जा सके। इन सामाजिक आंदोलनों की जगह जो परिवर्तन भारतीय समाज में आए उनका वर्णन निम्नलिखित है-
(i) सती-प्रथा का अंत (End of Sati System)-भारत में सती प्रथा सदियों से चली आ रही थी। अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जिंदा ही पति की चिता में जलना पड़ता था। इस अमानवीय प्रथा को ब्राह्मणों ने चलाया हुआ था। सामाजिक आंदोलनों की वजह से ब्रिटिश सरकार इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध हो गई तथा उसने 1829 में सती प्रथा विरोधी अधिनियम पास कर दिया तथा सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इस तरह सदियों से चली आ रही यह प्रथा खत्म हो गई। यह सब सामाजिक आंदोलन के कारण ही हुआ।
(ii) बाल-विवाह का खात्मा (End of Child Marriage)-बहुत-से कारणों की वजह से भारतीय समाज में बाल विवाह हो रहे थे। पैदा होते ही या 4-5 साल की उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था चाहे उन को विवाह का अर्थ पता हो या न हो। सामाजिक आंदोलनों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित कर दी। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बना कर विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष निश्चित कर दी।
(iii) विधवा-पुनर्विवाह (Widow Remarriage)-सदियों से हमारे समाज में विधवाओं को पुनर्विवाह की इजाजत नहीं थी। विधवाओं की स्थिति बहुत बद्तर थी। उनको किसी पारिवारिक समारोह में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। वह घुट-घुट कर मरती रहती थीं। उनको अपनी जिंदगी आराम से जीने का अधिकार नहीं था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों की वजह से अंग्रेजों ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया जिससे विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाजत मिल गई। इस तरह विधवाओं को कानूनी रूप से विवाह करने तथा अपनी जिंदगी आराम से जीने का अधिकार मिल गया।
(iv) पर्दा-प्रथा की समाप्ति (End of Purdah System)-मुस्लिमों में बरसों से पर्दा प्रथा चली आ रही थी। औरतों को हमेशा पर्दे के पीछे रहना पड़ता था। वही कहीं आ जा भी नहीं सकती थीं। यह प्रथा धीरे-धीरे सारे भारत में फैल गई। बड़े-बड़े समाज सुधारकों ने पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठायी। यहां तक कि सर सैय्यद अहमद खान ने भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठायी। इस तरह धीरे-धीरे पर्दा प्रथा कम होने लग गई तथा समय आने के साथ यह भी खत्म हो गई।
(v) दहेज-प्रथा में परिवर्तन (Change in Dowry System)-दहेज वह होता है जो विवाह के समय लड़की का पिता अपनी खुशी से लड़के वालों को देता था। धीरे-धीरे इसमें भी बुराइयां आनी शुरू हो गईं। लड़के वाले दहेज मांगने लगे जिस वजह से लड़की वालों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थीं। इसके विरुद्ध भी आंदोलन चले जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने तथा आज़ादी के बाद 1961 में सरकार ने दहेज लेने या देने को गैर-कानूनी घोषित कर दिया।
(vi) भारतीय समाज में बहुत समय से अस्पृश्यता चली आ रही थी। इसमें छोटी जातियों को स्पर्श भी नहीं किया जाता था। इन सामाजिक आंदोलनों में अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज़ उठी। जिस वजह से इसे गैर-कानूनी घोषित करने के लिए वातावरण तैयार हो गया तथा आजादी के बाद इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।
(vii) भारतीय समाज में अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध था। इन सामाजिक आंदोलनों की वजह से अंतर्जातीय विवाह को बल मिला जिस वजह से आजादी के बाद इसे भी कानूनी मंजूरी मिल गई।
(viii) इन आंदोलनों की वजह से भारतीय समाज के आधार जाति व्यवस्था पर गहरी चोट लगी। सभी आंदोलनों ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठायी जिस वजह से धीरे-धीरे जाति व्यवस्था खत्म होने लगी तथा आज भारत में जाति व्यवस्था अपनी आखिरी कगार पर खड़ी है।
(ix) सभी सामाजिक आंदोलन एक बात पर तो ज़रूर सहमत थे तथा वह थी स्त्री शिक्षा। हमारे समाज में स्त्रियों का स्तर काफ़ी निम्न था। उनको किसी भी चीज़ का अधिकार प्राप्त नहीं था। इन सभी आंदोलनों ने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किए जिस वजह से स्त्री शिक्षा को विशेष बल मिला। आज उसी वजह से स्त्री-पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी है।
इन सब चीजों को देखकर यह स्पष्ट है कि भारत में 19वीं सदी से शुरू हुए सामाजिक आंदोलनों की वजह से भारतीय समाज में बहुत-से परिवर्तन आए।
प्रश्न 2.
भारत में समाज सुधारक आंदोलन चलाने के लिए क्या सहायक हालात थे?
उत्तर:
भारत में सदियों से बहुत-सी कुरीतियां चली आ रही थीं। भारतीयों को इन कुरीतियों में पिसते-पिसते सदियां हो चली थी पर भारतीय इनमें पिसते ही जा रहे थे तथा इनके खिलाफ कोई आवाज़ भी उठ नहीं रही थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में अंग्रेजों ने भारत पर हकूमत करनी शुरू की। इसके साथ-साथ उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी शुरू किया।
भारतीयों ने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की तथा धीरे-धीरे उन्हें समझ आनी शुरू हो गई कि भारतीय समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं वह सब बेफिजूल की हैं जो कि ब्राहमणों ने अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए चलाई थीं। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर हकूमत करनी शुरू की तो उस समय भारत में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिनकी वजह से भारत में समाज सुधारक आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन हालातों का वर्णन निम्नलिखित है-
(i) पश्चिमी शिक्षा (Western Education)-अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी शुरू हुआ। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ उन्हें विज्ञान के बारे में यूरोप की प्रगति के बारे में भी पता चला। इस पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का यह असर हुआ कि उनको पता चलने लग गया कि उनके समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने देश में सामाजिक आंदोलन चलाने शुरू किए और सामाजिक परिवर्तन आने शुरू हो गए।
(ii) यातायात के साधनों का विकास (Development of Means of Transport)-अंग्रेजों ने भारत में चाहे अपने फायदे के लिए यातायात के साधनों का विकास किया पर उससे भारतीयों को भी बहुत फायदा हुआ। भारतीय इन यातायात के साधनों की वजह से एक-दूसरे के आगे आए तथा एक-दूसरे से मिलने लगे।
पश्चिमी शिक्षा ग्रहण चुके भारतीय भी देश के कोने-कोने पहुंचे तथा उन्होंने लोगों को समझाया कि यह सब प्रथाएं उनके फायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए हैं जिससे लोगों को यह समझ आने लग गया। इस तरह यातायात के साधनों के विकास के साथ भी आंदोलनों के लिए हालात विकसित हुए।
(iii) भारतीय प्रेस की शुरुआत (Indian Press)-अंग्रेजों के आने के बाद भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। आंदोलनों के संचालकों ने लोगों को समझाने के साथ छोटे-छोटे अखबार तथा पत्रिकाएं निकालनी भी शुरू की ताकि भारतीय इनको पढ़ कर समझ सकें कि ये बुराइयां हमारे समाज में कितनी गहरी पैठ बना चुकी हैं तथा इनको यहां से निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह प्रेस की शुरुआत ने भारतीयों को यह समझा दिया कि इन कुरीतियों को दूर करना कितना ज़रूरी है।
(iv) मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव (Increasing Effect of Missionaries)-जब से अंग्रेज़ भारत में आए रियों को भी सहायता देनी शरू की। अंग्रेज़ों ने इनको आर्थिक सहायता के साथ राजनीतिक सहायता भी देनी शुरू की। इन मिशनरियों का कार्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था पर इनका प्रचार करने का तरीका अलग था। वह पहले समाज कल्याण का कार्य करते थे। लोगों की तकलीफ दूर करते थे फिर इनमें ईसाई धर्म का प्रचार करते थे।
धीरे-धीरे लोग ईसाई धर्म को अपनाने लग गए। इससे समाज सुधारकों को बड़ी निराशा हुई क्योंकि भारतीय लोग अपना धर्म छोड़ कर विदेशी धर्म अपनाने लग गए थे। इन समाज सुधारकों ने भारतीयों को मिशनरियों के प्रभाव से बचाने के लिए समाज सुधारक आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। इस तरह ईसाई मिशनरियों के प्रभाव की वजह से भी यह आंदोलन शुरू हो गए।
कुप्रथाएं (So many ills in Indian Society)-जिस समय भारत में सुधार आंदोलन शुरू हुए उस समय भारतीय समाज में बहुत-सी कुप्रथाएं फैली हुई थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता इत्यादि कुप्रथाएं तथा इनके साथ जुड़े हुए बहुत से अंधविश्वास भी भारतीय समाज में फैले हुए थे। लोग भी इन सब से तंग आ चुके थे। जब यह आंदोलन शुरू हुए तो लोगों ने इन सुधारों को हाथों हाथ लिया जिस वजह से इन आंदोलनों को अच्छे हालात मिल गए तथा यह समाज सुधार के आंदोलन सफल हो गए।
प्रश्न 3.
भारतीय समाज सुधार आंदोलनों के नेताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? उनका वर्णन करें।
उत्तर:
वैसे तो भारत में समाज सुधार के बहुत से आंदोलन चले। इन आंदोलनों में बहुत से महान् व्यक्तियों ने भाग लिया। इन महान व्यक्तियों में से कुछ प्रमुख सुधारकों का वर्णन निम्नलिखित है-
(i) राजा राममोहन राय (Raja Ram Mohan Roy)-राजा राममोहन राय का नाम समाज सुधारकों में सबसे अग्रणी है। वह आधुनिक भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार के कार्य प्रारम्भ किए। इसलिए आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। उन्होंने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था। इसमें उन्होंने दनिया के अलग-अलग धर्मों को छोड़कर दुनिया के एक धर्म की स्थापना का विचार पेश किया। उस समय भारत में अमानवीय सती प्रथा प्रचलित थी।
उन्होंने अंग्रेजों को इस प्रथा के बारे में अवगत करवाया तथा उन्हीं के यत्नों से 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून पास किया। इसमें सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। इस तरह यह दर्दनाक प्रथा खत्म हो गई। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अंध-विश्वासों के कारण इनके खिलाफ आवाज़ उठाई।
उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जम कर आवाज़ उठाई। अपने अंतिम वर्षों में वह इंग्लैंड चले गए जहाँ 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय समाज के लिए उनका दिया योगदान अविस्मरणीय है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता।
(ii) देवेंद्रनाथ ठाकुर (Devendera Nath Thakur)-राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि ब्रह्म समाज खत्म हो जाएगा पर 1845 में ब्रह्म समाज का भार देवेंद्रनाथ ठाकुर ने अपने हाथों में ले लिया तथा वह इसके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। 1839 में उन्होंने तत्त्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा इस सभा का लक्ष्य उन्होंने सत्य की शिक्षा देना रखा।
वह तत्त्वबोधिनी पत्रिका के संपादक भी रहे। 1847 में इस सभा ने ऋग्वेद का अनुवाद भी किया। 1847 में ही वह बनारस गए तथा उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। उन्होंने राजा राममोहन राय की तरह विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा पर काफ़ी ज़ोर दिर इनकी मृत्यु हो गई थी।
(iii) केशवचंद्र सेन (Keshav Chandra Sen) केशवचंद्र सेन ने 1861 में ब्रह्म समाज के कार्यों में ध्यान देना शुरू किया तथा संगीत सभा की स्थापना की। आपने 1861 में Indian Mirror नामक पत्रिका प्रकाशित की। इस पत्रिका की मदद से ही उन्होंने अपने समाज सुधार के आंदोलन को आगे बढ़ाया।
आपने 1863 में ‘वामा बोधिनी’ नामक पत्रिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए तथा अंतर्जातीय विवाह का प्रचार किया। 1868 में आपने ब्रह्म समाज के संदेश घर-घर तक पहुंचाने के लिए ‘भारतवर्ष ब्रहम समाज’ की स्थापना की। 1884 में आपका देहांत हो गया।
(iv) स्वामी दयानंद सरस्वती (Swami Dayanand Saraswati)-आपका जन्म सन् 1824 में हुआ था। आपका पहला या असली नाम मूलशंकर था। आपने 24 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया तथा अलग-अलग शहरों में घूमकर अपने उपदेशों का प्रचार किया।
1871 से 1873 आप गंगा किनारे घूमते रहे तथा स्कूलों का प्रब करते रहे। 1874 में आपने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया तथा 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आपने पंजाब में जगह-जगह आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक, धर्म परिवर्तन को रोकने के विरुद्ध आवाज़ उठाई।
आपके द्वारा दयानंद वैदिक संस्थाओं की स्थापना की गई तथा इसमें सिर्फ भारतीय ही पढ़ा सकते थे। इन संस्थाओं में नैतिक शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया गया। आपने जाति प्रथा का विरोध किया। आपके यत्नों से ही हिंदू धर्म छोड़ चुके लोग वापस हिंदू धर्म को अपनाने लग गए। आपके यत्नों से ही अंतर्जातीय विवाह शुरू हो गए। 1883 में आपका निधन हो गया।
(v) स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda)-आप स्वामी रामकृष्ण के परम शिष्य थे। आपने 1883 में शिकागो में हई Parliament of Religion में भाग लिया। वहां पर आपने जो अपने विचार प्रस्तुत किए उनसे उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हो गई। आपने उस सभा में वेदों की शिक्षा संबंधी बात की तथा आपकी बातें सुनने के पश्चात् लोगों को लगने लग गया कि उस सभा में आप ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं।
आप कहते थे कि ईश्वर एक है तथा सर्वव्यापक है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बसता है। जब मनुष्य अपने आप पर काबू पा लेता है तो वह पूर्ण हो जाता है तथा भगवान् को प्राप्त कर लेता है। सारा संसार धर्म के ऊपर तथा धर्म के अनुसार ही चलता है। आपने राजा राममोहन राय की तरह विश्व धर्म की बात की जिसने भारतीयों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्रभावित किया। आपके विचारों से प्रभावित होकर आपके शिष्यों की गिनती बढ़ती चली गई।
आपने अस्पृश्यता तथा जाति प्रथा के विरुद्ध जम कर प्रचार किया तथा आप चाहते थे कि अलग-अलग धर्मों तथा जातियों में एकता बनी रहे। आपने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ताकि धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इस मिशन की मदद से आपने शिक्षा का प्रसार, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, पशु पालन, अनाथालय, स्कूलों कॉलेजों की स्थापना की तथा देशवासियों को पुनर्जीवित करने तथा जाति-पाति के भेदभाव मिटाने के प्रयास किए। आपकी मृत्यु 1902 में हो गई थी।
प्रश्न 4.
भारत में महिलाओं में चले सुधार आंदोलन का वर्णन करो।
उत्तर:
भारतीय समाज में समय-समय पर अनेक ऐसे आंदोलन शुरू हुए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों की दशा में सुधार करना रहा है। भारतीय समाज एक पुरुष-प्रधान समाज है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं ने अपने शोषण, उत्पीड़न इत्यादि के लिए अपनी स्थिति में सुधार के लिए आवाज़ उठाई है। पारंपरिक समय से ही महिलाएं बाल-विवाह, सती–प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का शिकार होती आई हैं।
महिलाओं को इन सब शोषणात्मक कुप्रथाओं से छुटकारा दिलवाने के देश के समाज सुधारकों ने समय-समय पर आंदोलन चलाये हैं। इन आंदोलनों में समाज सुधारक तथा उनके द्वारा किये गए प्रयास सराहनीय रहे हैं। इन आंदोलनों की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हो गई थी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशवचंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऐनी बेसेंट इत्यादि का नाम इन समाज सुधारकों में अग्रगण्य है।
सन् 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना तथा 1829 में सती प्रथा अधिनियम का बनाया जाना उन्हीं का प्रयास रहा है। स्त्रियों के शोषण के रूप में पाये जाने वाले बाल-विवाह पर रोक तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित कराने का जनमत भी उन्हीं का अथक प्रयास रहा है। इसी तरह महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र, विदयासागर जी ने भी कई ऐसे ही प्रयास किये जिनका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ा है।
महर्षि कर्वे स्त्री-शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के समर्थक रहे । इसी प्रकार केशवचंद्र सेन एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के अंतर्गत ही 1872 में ‘विशेष विवाह अधिनियम’ तथा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इन अधिनियमों के आधार पर ही विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई। इनके साथ ही कई महिला संगठनों ने भी महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए कई आंदोलन शुरू किये।
महिला आंदोलनकारियों में ऐनी बेसेंट, मैडम कामा, रामाबाई रानाडे, मारग्रेट नोबल आदि की भूमिका प्रमुख रही है। भारतीय समाज में महिलाओं को संगठित करने तथा उनमें अधिकारों के प्रति साहस दिखा सकने का कार्य अहिल्याबाई व लक्ष्मीबाई ने प्रारंभ से किया था। भारत में कर्नाटक में पंडिता रामाबाई ने 1878 में स्वतंत्रता से पूर्व पहला आंदोलन शुरू किया था तथा सरोज नलिनी की भी अहम् भूमिका रही है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रचलित इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप ही अनेक ऐसे अधिनियम पास किये गए जिनका महिलाओं की स्थिा स्थति सधार में योगदान रहा है। इसी प्रयास के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात अनेक अधिनियम जिनमें 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम एवं 1961 का दहेज निरोधक अधिनियम प्रमुख रहे हैं।
इन्हीं अधिनियमों के तहत स्त्री-पुरुष को विवाह के संबंध में समान अधिकार दिये गए तथा स्त्रियों को पृथक्करण, विवाह-विच्छेद एवं विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार संपूर्ण भारतीय समाज में समय-समय पर और भी ऐसे कई आंदोलन चलाए गए हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य स्त्रियों को शोषण का शिकार होने से बचाना रहा है।
वर्तमान समय में स्त्री-पुरुष के समान स्थान व अधिकार पाने के लिए कई आंदोलनों के माध्यम से एक लंबा रास्ता तय करके ही पहुंच पाई है। समय-समय पर राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा महिला संगठनों के प्रयासों के आधार पर ही वर्तमान महिला जागृत हो पाई है। इन सब प्रथाओं के परिणामस्वरूप ही 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया।
इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में महिला विकास निगम [Women Development Council (WDC)] का निर्माण किया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को तकनीकी सलाह देना तथा बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण इत्यादि दिलवाना है। वर्तमान समय में अनेक महिलाएं सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आज स्त्री सभी वह कार्य कर रही है जो कि एक पुरुष करता है।
महिलाओं के अध्ययन के आधार पर भी वह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में महिला की परिस्थिति, परिवार में भूमिका, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक एवं कानूनी भागीदारी में काफ़ी परिवर्तन आया है। आज महिला स्वतंत्र रूप से किसी भी आंदोलन, संस्था एवं संगठन से अपने आप को जोड़ सकती है। महिलाओं की विचारधारा में इस प्रकार के परिवर्तन अनेक महिला स्थिति सुधारक आंदोलनों के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाये हैं।
आज महिला पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं तथा इसके साथ ही महिला सभाओं एवं गोष्ठियों का भी संचालन किया जा रहा है जिसका प्रभाव महिला की स्थिति पर पूर्ण रूप से सकारात्मक पड़ रहा है। विभिन्न महिला आंदोलनों ने न केवल महिलाओं की स्थिति सुधार में ही भूमिका निभाई है, बल्कि इन आंदोलनों के आधार पर समाज में अनेक परिवर्तन भी आये हैं, अतः महिला आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का भी एक उपागम रहा है।

प्रश्न 5.
ब्रह्म समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके उद्देश्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन करो।
अथवा
ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
ब्रह्म समाज (Brahmo Smaj)-ब्रह्म समाज की स्थापना आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त, 1828 ई० में की। ब्रह्म समाज का शाब्दिक अर्थ है “एक ईश्वर समाज” यह समाज मूल रूप से ब्राह्मणों का समाज था जिसमें अन्य जातियों के लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके कार्यकाल में निरंतर वृधि होती गई जिसके कारण ब्रह्म समाज के कार्यक्रमों में अन्य जातियों के लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लेना आरंभ कर दिया।
राजा राममोहन राय के पश्चात् देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशवचंद्र सेन आदि समाज सुधारकों ने ब्रह्म समाज को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में लघु पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, सभाओं एवं गोष्ठियों के माध्यम से इसका प्रचार एवं प्रसार किया। परिणामस्वरूप पहले 1866 तक केवल 54 ब्रह्म समाज स्थापित हुए थे जिनकी संख्या 1911 में बढ़कर 184 हो गई।
उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज में अनेक बुराइयां, कुरीतियां, अंध-विश्वास एवं कुसंस्कार प्रचलित थे। बाल-विवाह की संख्या अधिक थी। विधवा विवाह पर रोक थी। सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफ़ी निम्न व कमज़ोर थी। जाति प्रथा, छुआछूत, जाति के आधार पर उच्च जातियों को विशेषाधिकार तथा निम्न जाति व वर्गों के लोगों को कम ही सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने दिया जाता था।
यह उस समय भारतीय समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा थी। विभिन्न वर्गों के सदस्यों को इन कुरीतियों से छुटकारा दिलवाना आवश्यक था। ब्रह्म समाज की स्थापना तथा इसके सिद्धांतों को कार्यांवित कर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति इसी दिशा में एक बड़ा कदम था।
ब्रह्म समाज के उद्देश्य (Objectives of Brahmo Smaj)-ब्रह्म समाज के उद्देश्य निम्नलिखित हैं
- नारी वर्ग का उत्थान करना।
- बाल विवाह एवं बहु-विवाह को समाप्त करना।
- सती प्रथा का अंत करना।
- पर्दा प्रथा का अंत करना।
- नारी शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना।
- अस्पृश्यता तथा जाति प्रथा के अन्य दोषों को समाप्त करना।
- ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन करना।
- मानवतावाद को बढ़ावा देना।
- सेना तथा न्यायपालिका का भारतीयकरण करने के लिए कार्य करना।
ब्रहम समाज के कार्य एवं उपलब्धियां (Works and Achievements of Brahmo Smaj) विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्रह्म समाजी मुख्यतः तीन स्तरों पर अपनी गतिविधियां संचालित करते थे। प्रथम, देश के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाजों की स्थापना कर, उनमें संगठन के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के ऊपर विचार करना, द्वितीय, अपने सिद्धांतों का लोगों में प्रचार एवं प्रसार करते थे।
तृतीय, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से सहयोग पाते थे। ब्रह्म समाजी के लोग विभिन्न स्थानों पर बैठकें करते थे। सम्मेलनों व संगोष्ठियों का आयोजन करते थे। अपने सिद्धांतों को जन-जन में पहुँचाने के लिए लघु पुस्तिकाएं छपवा कर उनमें बांटते थे। अपने सुधारवादी कार्यों के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूकता का विकास करते थे। सन् 1829 में अपने अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार से ‘सती प्रथा’ के विरुद्ध कानून पास करवाया।
इसी तरह 1872 ई० में बहु विवाह प्रथा पर भी प्रतिबंध लगवाने हेतु कानून पारित करवाया। इसी तरह बाल-विवाह व पर्दा प्रथा को कम करने के लिए सफल प्रयास करवाया। लोगों में जातीय आधार पर भेदभाव कम करने के प्रति जनसमर्थन को बढ़ावा दिया। नारी शिक्षा हेतु ब्रह्म समाज ने सराहनीय कार्य किये। इसी तरह लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। लोगों को आध्यात्मिक विकास हेतु प्रेरणा दी। इसी तरह भारतीय समाज में पाई जाने वाली कई सामाजिक बुराइयों को कम करने में ब्रह्म समाज का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
प्रश्न 6.
आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी उपलब्धियों का वर्णन करो।
अथवा
आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर:
आर्य समाज (Arya Smaj)-सन् 1875 ई० में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता, आडंबरों, पाखंडों तथा अज्ञानता को दूर करना था। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज विशेषतः हिंदू समाज में कई प्रकार की बुराइयां विकसित हो गई। उस समय धार्मिक क्षेत्रों में अनेक देवताओं की पूजा की जाती थी।
इस तरह अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग आपस में नफरत व द्वेष रखते थे। ईसाई मिशनरी हिंदुओं में धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें ईसाई बनाने में लगी थी। जाति व्यवस्था भी काफ़ी जटिल हो गई थी। समाज सहस्रों जातियों एवं उपजातियों में विभाजित था। जातीय आधार पर विभिन्न वर्गों में भेदभाव बढ़ गया था। स्त्रियों से संबंधित अनेक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, नवजात लड़कियों की हत्या तथा दहेज के कारण महिलाओं की काफ़ी निम्न अवस्था आदि प्रचलित थीं। इन समस्याओं का निराकरण आवश्यक था।
आर्य समाज के कार्य व उपलब्धियां (Works and Achievements of Arya Smaj)-आर्य समाज ने अपनी स्थापना के 125 वर्षों के भीतर भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधारवादी कार्य किये। समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को कम करने के लिए कार्य किये। इसके लिए ‘कन्या विद्यालयों’ एवं ‘कन्या महाविद्यालयों’ की स्थापना करवाई, ताकि उनमें ज्ञानरूपी प्रकाश जलाकर अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर किया जा सके।
विधवाओं की स्थिति सुधारने हेतु कई ‘विधवा ग्रह’ (Widow Home) खोले गये, ताकि वहाँ पर विधवाएं जिंदगी व्यतीत कर सके। वेदों के अनुसार हवन, यज्ञ करने और करवाने, वेदों को सुनने एवं सुनाने पर बल दिया गया। जाति के आधार पर असमानता का विरोध किया गया। धार्मिक क्षेत्रों में वेदों की वापसी (Back to Vedas) का नारा देकर लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया गया।
अनाथों के लिये ‘अनाथालय’ खोले: ऐग्लो वैदिक (Dayanand Anglo Vedic-D.A.V.) पाठशालाएं एवं महाविद्यालय (Universities) की स्थापना की गई। उपरोक्त शिक्षा क्षेत्र में आर्य समाज ने सराहनीय कार्य किये। इससे न केवल देश की साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी च शिक्षा प्राप्त करके हज़ारों नवयुवक देश की सेवा के लिये तैयार हो गये। स्वामी दयानंद सरस्वती देश की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने नारा दिया “भारत, भारतवासियों के लिए है।”
प्रश्न 7.
प्रार्थना समाज के उद्देश्यों तथा उपलब्धियों का वर्णन करो।
उत्तर:
प्रार्थना समाज (Prathna Smaj)-सन् 1867 ई० में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, यह मूलतः ब्रह्म समाज की एक शाखा ही थी जिसकी स्थापना केशवचंद्र की सहायता से (प्रेरणा से) गोविंद रानाडे के नेतृत्व में की गई। महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के अनेक नेताओं ने प्रार्थना समाज की नींव डालने व इसे निश्चित स्वरूप करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। प्रार्थना समाज के अनुयायी इसे हिंदू धर्म में ही एक आंदोलन मानते थे जिस पर अनेक संतों जैसे ‘तुकाराम’, ‘नामदेव’ व ‘रामदास’ का गहरा प्रभाव था।
प्रार्थना समाज के उद्देश्य (Objectives of Prarthna Smaj):
- प्रार्थना समाज की शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार करना।
- स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना।
- जातीय भेदों को दूर करना।
- अनाथों की स्थिति में सुधार करना।
- शिक्षा को प्रोत्साहन करना।
प्रार्थना समाज के कार्य व उपलब्धियां-(Works and Achievements of Prarthna Smaj):
प्रार्थना समाज के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों को सुधारने तथा कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की गई है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में किये कार्यों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है-
- महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए ‘आर्य महिला समाज’ की स्थापना की। विधवा आश्रम खोले, कन्या पाठशालाओं की स्थापना की।
- विधवा पुनर्विवाह व अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किये।
- निम्न जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से दलित वर्ग मिशन की स्थापना की।
- अनाथों एवं बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए पंठरपुर में अनाथालय खोले गये। बाल विवाह को कम करने के लिये निरंतर प्रयास किये गये हैं।
- मुंबई में रात्रि-विद्यालय (Night School) खोला गया ताकि मजदूर वर्ग शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरह प्रार्थना समाज ने अंतर्जातीय भेदभाव दूर करने के लिये अंतर्जातीय खान-पान को बढ़ावा दिया गया।
प्रश्न 8.
राम कृष्ण मिशन के उद्देश्यों तथा कार्यों का वर्णन करो।
अथवा
रामकृष्ण मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
राम कृष्ण मिशन (Ram Krishna Mission)-सन् 1897 ई० में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के निकट वैलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त एवं प्रिय शिष्य थे। विवेकानंद ने अपने गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस मिशन की स्थापना की। कुशाग्र बुद्धि, मन-मोहक व्यक्तित्व, मधुर वाणी तथा धारा प्रवाह वक्ता दयानंद ने देश व विदेश में इस मिशन की शाखाओं की स्थापना की।
कुशल प्रचारक व संगठक (Organisor) होने के कारण उन्होंने सन् 1902 में अपनी मृत्यु से पहले ही इस मिशन की नींव काफ़ी मज़बूत कर दी थी। उनके पश्चात् भी मिशन के कार्यकर्ताओं ने इसके प्रचार व प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि सन् 1961 में इस मिशन की भारत में 102 शाखाएं तथा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यनमार (बर्मा), फिजी तथा मोरिशस आदि विश्व के विभिन्न देशों में 36 शाखाएँ थीं।
राम कृष्ण मिशन के उद्देश्य (Objectives of Ram Krishna Mission)-इस मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- आत्मत्यागी तथा व्यावहारिक अध्यात्मवादी साधुओं को रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के प्रचार व प्रसार के लिये तैयार करना।
- सभी जाति व संप्रदायों के लोगों से दयायुक्त, दानयुक्त तथा मानवीय कार्य करवाना।
- सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों को समाप्त करना।
- स्त्रियों का स्थान उच्च करने के लिए कार्य करना।
- सेवा के सिद्धांत (सब जीवन मात्र की सेवा) का प्रचार करना।
- मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना।
राम कृष्ण मिशन के कार्य, उपलब्धियां एवं योगदान (Works, Achievements and Contribution of Ram Krishna Mission)-राम कृष्ण मिशन के कार्यों एवं समाज सुधार में इसके योगदान का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है-
- शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह-जगह पाठशालाएं एवं महाविद्यालय खोले गये। सन् 1961 में मिशन द्वारा खोले गये शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 65 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।
- स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक अस्पताल खोले। सन् 1961 ई० में मिशन द्वारा संचालित बारह शैयायुक्त अस्पताल तथा 68 बाह्य रोगी (Outdoor Patient) अस्पताल थे।
- मिशन के सिद्धांतों के प्रचार के लिये अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में लगभग एक दर्जन पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं।
- मिशन द्वारा सभाओं, संगोष्ठियों, लेखों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से बाल-विवाह, बाल हत्या, पर्दा प्रथा, जातीय आधार पर भेदभाव तथा स्त्री-पुरुष में असमानता का कड़ा विरोध किया जाता है। फलतः लोगों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आत्मत्याग, आत्मसम्मान, परोपकार आदि भावनाओं का संचार हुआ।
- लोगों में अंधविश्वासों, कुरीतियों, पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के विरुद्ध जागृति आई। देशवासियों में देश प्रेम व राष्ट्रवाद की भावना भी विकसित हुई।
- मिशन ने समय-समय पर बाढ़ पीड़ितों, भूकंप प्रभावित तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लाखों लोगों की सहायता की।
राम कृष्ण मिशन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के बारे में डॉ० के० के० दत्ता कहते हैं, “राम कृष्ण मिश आध्यात्मिक उत्थान, आत्मा की जागृति और आधुनिक भारत के सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, इस संसार को मानव समाज में धर्म के सही महत्त्व का ज्ञान प्राप्त हुआ तथा विभिन्न देशों को प्यार, स्वतंत्रता तथा एक सूर का संदेश मिला।”
प्रश्न 9.
पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं?
अथवा
पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? उनका वर्णन करो।
अथवा
भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों की व्याख्या करें।
अथवा
पश्चिमीकरण के प्रभाव बताइए।
उत्तर:
पश्चिमीकरण ने भारतवर्ष को काफ़ी ज्यादा प्रभावित किया है। भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जो पश्चिमीकरण से प्रभावित न हुआ होगा। इस तरह भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का वर्णन निम्नलिखित है-
1. परिवार पर प्रभाव-पारंपरिक रूप से भारत में संयुक्त परिवार पाए जाते रहे हैं जिनमें तीन-चार पीढ़ियां इकट्ठी रहती थीं। पश्चिमीकरण से भारत में व्यक्तिवाद, भौतिकवाद तथा तर्कवाद को बढ़ावा मिला। इससे परिवार में समूहवाद में कमी आई। परिवार के सदस्यों में बलिदान तथा त्याग की भावना कम हुई। शिक्षित युवाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी।
उन्होंने कर्ता के आदेशों को मानना कम किया। महिलाओं में भी अपने लिए पहचान बनाए रखने के लिए चेतना बढ़ी है। महिलाओं तथा युवाओं में आई चेतना की वजह से संयुक्त परिवार तेज़ गति से टूटने लगे। इनकी जगह केंद्रीय परिवार लने लगे। इस तरह पश्चिमीकरण से परिवार व्यवस्था पर संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक प्रभाव पड़े। परिवार के सदस्यों के संबंधों के स्वरूप, अधिकारों तथा दायित्व में परिवर्तन हुआ।
2. विवाह पर प्रभाव-इंग्लैंड के निवासियों के विचारों, मूल्यों और आदर्शों ने भारतीय विवाह प्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया। इनके भारत आने से पहले अंतर्विवाही प्रथा, विधवा विवाह की मनाही, बाल विवाह, कुलीन विवाह तथा कन्यादान का प्रथा थी। विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। विवाह में सपिंड, सगोत्र व सप्रवर के नियमों का पालन होता था तथा तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
परंतु पश्चिम के विचारों, मूल्यों तथा आदर्शों की वजह से विवाह के कई नियमों में परिवर्तन हुए। बाल विवाह पर रोक लगाना तथा देरी से विवाह करना, विधवाओं को दोबारा विवाह की छूट, प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा तथा कोर्ट मैरिज होने लगी, तलाकों की गिनती में बढ़ोत्तरी हुई तथा कुलीन तथा बहुविवाह की संख्या में कमी आई। एक विवाह को ही ठीक माना जाने लगा। पश्चिमीकरण के कारण विवाह अब एक समझौता मात्र बन कर रह गया है। प्रेम विवाह तथा कोर्ट मैरिज के बढ़ने के साथ-साथ तलाकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
3. नातेदारी पर प्रभाव (Impact on Kinship)-भारतीय समाज में नातेदारी की मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका रहती है। मगर पश्चिमीकरण के कारण व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, गतिशीलता तथा समय धन है, आदि अवधारणाओं का भारतीय संस्कृति में तीव्र विकास हआ। इससे ‘विवाह मलक’ तथा ‘रक्त मूलक’ (Affinal & Consaguineoun) दोनों प्रकार की नातेदारियों पर प्रभाव पड़ा।
द्वितीयक एवं तृतीयक (Secondary & Tertiary) संबंध शिथिल पड़ने लगे।प्रेम विवाहों तथा कोर्ट विवाहों में विवाहमूलक नेतादारी कमज़ोर पड़ने लगी। विवाह, जन्म दिवस तथा उत्सवों पर नातेदारी का स्थान मित्र मंडली एवं सहकर्मी लेने लगे। पश्चिमी समाजों में नातेदारी को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता।
इसलिए अनेक समानांतर संबंधियों को एक ही शब्द से संबोधित किया जाता है। इन शब्दों का भारतीय समाज में बढ़ता प्रचलन नातेदारी के महत्त्व में परिवर्तनों का द्योतक है, जैसे चाचा, ताया, फूफा, मौसा तथा मामा पांच अलग-अलग संबंधी हैं, जिनके लिये अंकल (Uncle) शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। इस तरह चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई-बहिनों को (Cousin) कहा जाने लगा है।
4. जाति प्रथा पर प्रभाव (Impact on Caste System) सहस्त्रों वर्षों से भारतीय समाज की प्रमुख संस्था, जाति में पश्चिमीकरण के कारण अनेक परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये और यातायात तथा संचार के साधनों जैसे-बस, रेल, रिक्शा, ट्राम इत्यादि का विकास व प्रसार किया। इसके साथ-साथ भारतीयों को डाक, तार, टेलीविज़न, अखबारों, प्रेस, सड़कों व वायुयान आदि सुविधाओं को परिचित कराया।
बड़े साथ उद्योगों की स्थापना की गई। इनके कारण विभिन्न जातियों के लोग एक स्थान पर उद्योग में कार्य करने लग गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आधुनिक यातायात के साधनों का प्रयोग होने लगा। इससे उच्चता व निम्नता की भावना में भी कमी आने लगी। एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के व्यवसाय को अपनाने लग गए। सेवाओं के बदले अनाज के स्थान पर पैसे दिये जाने लगे और पैसे के आधार पर दूसरी जाति के सदस्यों की सेवाएं ली जाने लगीं।
एक साथ काम करने के कारण खान-पान संबंधी जातीय प्रतिबंध भी कमज़ोर पड़ने लगे। भारतीय समाज में जातीय आधार पर पंचायतों के गठन के स्वरूप में भी कमी आई। पश्चिम के समानता के मूल्यों एवं वैज्ञानिक ज्ञान ने भारतीय समाज में जातीय भेदभाव को कम किया तथा समानता के विचारों का प्रसार किया।
5. अस्पृश्यता (Untouchability)-अस्पृश्यता भारतीय जाति व्यवस्था का अभिन्न अंग रही थी। मगर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित पश्चिमी मूल्यों ने जातीय भेदभाव को कम किया। जाति तथा धर्म पर भेदभाव किये बिना सभी के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की अनुमति, सभी के लिये एक जैसी शिक्षा व्यवस्था, समान योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिये समान नौकरियों पर नियुक्ति आदि कारकों से अस्पृश्यता में कमी आई। अंग्रेज़ों ने औद्योगीकरण व नगरीयकरण को बढ़ावा दिया। विभिन्न जातियों के लोग रेस्टोरेंट, क्लबों में एक साथ खाने-पीने एवं बैठने लग गए। अतः पश्चिमीकरण के कारण भारत में अस्पृश्यता में कमी आई।
6. धार्मिक जीवन पर प्रभाव (Impact on Religious life)-भारत में अंग्रेज़ी शासन से पूर्व अनेक धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों, पाखंडों आदि का प्रचलन था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव एवं इसाई धर्म प्रचारकों के धर्म प्रचार के कारण धार्मिक एवं सुधारवादी अंदोलन आरंभ किये गए। इन सबके कारण बहुत से धार्मिक अंधविश्वास एवं धार्मिक बुराइयां समाप्त हो गईं।
कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर अपने आपको ईसाई बना लिया। हिंदू धर्म में भी समानतावाद व मानवतावाद आदि तत्त्वों को बढ़ावा मिला। अतः पश्चिमी प्रभाव के कारण कई बुराइयों का अंत हुआ। इसके साथ ही लोगों में धार्मिक विश्वासों एवं प्रभाव में कमी आई। हिंदू धर्म में धर्मांधता में कमी आई तथा धर्म में तर्कवाद तथा ईसाई धर्म का भारतीयकरण हुआ।
7. स्त्रियों की प्रस्थिति में परिवर्तन (Change in Status of Women)-अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय भारत में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न थी। सती प्रथा पर्दा प्रथा तथा बाल-विवाह का प्रचलन था तथा विधवा पनर्विवाह पर रोक होने के कारण महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया तथा विधवा विवाह को पुनः अनुमति दी। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार व प्रचार के माध्यम से चूंघट प्रथा में कमी आई।
पश्चिमीकृत महिलाओं ने पैंट-कमीज़ पहननी आरंभ की। लाखों महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आई और उन्होंने केवल घर को संभालने की पारंपरिक भूमिका को त्यागकर पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर दफ्तरों में विभिन्न पदों पर नौकरी करनी आरंभ कर दी। इस तरह स्त्रियां अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में सफ़ल हुई।
8. शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव (Impact in the field of Education)-भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली पर भी पश्चिम का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने से पूर्व यहां शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी तथा शिक्षा सभी लोगों के लिये उपलब्ध नहीं थी। शैक्षणिक संस्थाओं में संस्थाओं में साधारणतया उच्च जाति के लोग ही प्रवेश कर सकते थे, निम्न जाति के लोगों को पाठशालाओं में शिक्षा की अनुमति नहीं थी, अगर पिछड़ी जाति के लोग शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला ले भी लेते थे तो उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था।
लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी संस्थाएं स्थापित की गई तथा साथ ही सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली आरंभ की गई जिसमें सभी जातियों एवं वर्गों के लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे। लार्ड मैकाले ने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय एवं प्रशासनिक सेवा में प्राथमिकता दी जाने लगी।
इस शिक्षा ग्रहण उपरांत भारतीयों के विचारों, मूल्यों, आदर्शों व जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन आये। अंग्रेजी शिक्षा ने ही भारतीयों में राष्ट्रीयता एकता व समानता की भावना विकसित की। वर्तमान समय में कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि की दी जाने वाली शिक्षा व परीक्षण अंग्रेज़ी शिक्षा की ही देन है।
9. सामाजिक आदर्श व मूल्यों पर प्रभाव (Impact on Social Norms and Values) लोक रीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं, प्रथाओं, नियमों, कानूनों एवं व्यवहारों के तरीकों, विश्वासों, शिष्टाचारों, अनुष्ठानों, मूल्यों, कलाओं तथा साहित्य के रूप में भारतीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। अंग्रेज़ों के भारत में शासन स्थापित करने तथा ब्रिटेन वासियों के भारतवासियों के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क बढ़ने से इन सांस्कृतिक तत्त्वों में काफ़ी परिवर्तन आये।
इनका पश्चिमीकरण हुआ। अभिवादन करने में चरण-स्पर्श व प्रणाम का स्थान हाथ मिलाना, गुड मार्निंग करना ले रहे हैं। प्रथाओं को कानून का चोला पहनाया जा रहा है। जैसे-सती प्रथा को कानूनी अवैध करार दिया गया। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। विवाह, जन्म दिन तथा अन्य उत्सवों पर नातेदारियों, सगे संबंधियों, मित्रों तथा अन्य लोगों को उनके घर स्वतः जाकर आमंत्रित करने को अपेक्षा निमंत्रण कार्ड (Invitation-Card) देकर निमंत्रण दिया जाने लगा।
10. जीवन शैली पर प्रभाव (Impact on Way of life)-भारत की जीवन पद्धति पर पश्चिम का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बड़े-बड़े नगरों व शहरों में रिक्शाचालकों तक अंग्रेजी बोलते हुए देखे गये हैं। पहले यहां पर धोती-कुर्ता या पजामा पहना जाता था, वहीं आजकल कोट, पैंट, बुशर्ट, टाई, मौजा ही पहनने लगे। अंग्रेज़ी फ़ैशन ने भारतीय फैशन पर अपना काफ़ी रंग चढ़ाया। महिलाओं में ऊंची ऐड़ी के सैंडिल, साड़ी, ब्लाऊज, जीन तथा मैकसी, इत्यादि का प्रयोग होता है।
समाज में शिक्षित लोग मकानों की सजावट व बनावट-रहन सहन के ढंग तथा उत्सवों या पार्टियों आदि में पश्चिमी मान्यताओं का अनुकरण करते हुए देखे जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का भी अधिकाधिक प्रयोग प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। अब लोग विलासता को वस्तुएं, टेलीविज़न, फ्रिज, टेप रिकार्ड, कपड़े धोने की मशीन, कार आदि को भी अपने जीवन का अंग बना रहे हैं। अंग्रेजी संगीत में बढ़ती हुई रुचि, क्लब संस्कृति का प्रसार, पश्चिमी तरीकों से पार्टियों का आयोजन, छुरी और कांटों से मेज पर बैठकर भोजन करना, पश्चिमी जीवन शैली के बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाता
11. भाषाओं पर प्रभाव (Impact on Languages)-सन् 1835 में लार्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू किया। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन के दौरान तथा स्वतंत्रोपरांत भारत में निरंतर अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ता गया। यद्यपि अंग्रेज़ी-संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 18 भाषाओं में से नहीं है। इसे संपर्क भाषा (link language) के रूप में अपनाया गया है।
मगर वर्तमान समय में देश की अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं तथा विशेषतः विश्वविद्यालयों तथा महाविश्वविद्यालयों में या तो अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाता है या फिर विज्ञान, इंजीनियरिंग मैडीकल तथा व्यावसायिक कोरों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है। आधुनिक प्रजातंत्र, संसदीय प्रणाली तथा वर्तमान नौकरशाही तथा नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकार अंग्रेजों की ही देन हैं।
12. विश्वास एवं शिष्टाचार (Beliefs and Etiquettes)-प्राचीन काल से भारतीय समाज के अपने विशिष्ट विश्वास एवं शिष्टाचार रहे है। पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने से इनमें अंतर आया है। पौराणिक काल से भारतीय समाज में चंद्रमा एवं सूर्य का मानवीकरण करके इन्हें शक्तियों के रूप में माना जाता रहा है। ये विश्वास किया जाता रहा कि राहू और केतू के दोनों तरफ से घेर लेने के कारण सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) लगता है तथा ग्रहण के समय सूर्य घोर संकट में होता है।
मगर पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान के भारत में प्रसार से शिक्षित वर्ग में यह वैज्ञानिक मान्यता के रूप में विकसित हुई है कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र है जिसमें चंद्रमा के सूर्य एवं पृथ्वी की रेखा में आने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने से रुक जाती है। शिष्टाचारों का भी पश्चिमीकरण हुआ है। चरण-स्पर्श, तथा दंडवत् करने के स्थान पर हाथ मिलाना, अतिथि को दूध-लस्सी के बजाए ठंडा पेय या काफ़ी देना आदि सभ्याचार भारत में पश्चिमीकरण के कारण ही है।
13. नव-प्रौद्योगिकी लागू करना (Introducting of New Technology)-अंग्रेजों ने भारत में नव शिल्पास्त्र लागू किया। उन्नत तकनीक के भारत में लागू करने से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं लोगों की जीवन-शैली में कई परिवर्तन आये। उन्होंने रेलों का विकास किया (सन् 1853 में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ की। सड़कों का निर्माण किया, प्रेस विकसित की। घरेलू उपयोग के लिये स्टील के बर्तन बनाये।
बसों, रेलों, तथा जहाजों का निर्माण तथा डाक-तार एवं छापखाने (Printing press) के विकास से यातायात एवं दूरसंचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लोगों ने पारंपरिक रूप से भूमि पर बैठकर पत्ती में खाना खाने की जगह कुर्सी-मेज पर बैठकर स्टील की थाली प्लेट में चम्मच-छुरी-कांटे के साथ खाना आरंभ किया।
औदयोगीकरण (Industrialisation) अंग्रेजों ने भारत में अपने शासनकाल के आरंभ में ही यहां की अमूल्य वस्तुओं तथा कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाना प्रारंभ किया। अपने देश में इस कच्चे माल से नई-नई वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें भारत में बेचना आरंभ कर दिया। उन्नत तकनीक से मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती एवं अधिक गुणवत्ता वाली होती थीं। जबकि भारतीयों द्वारा भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग में निर्मित वस्तुएं अपेक्षाकृत महंगी तथा कम गुणवत्ता वाली होती थी।
फलस्वरूप भारतीय उद्योग को काफ़ी धक्का लगा। ज़मींदारी व्यवस्था लागू करने एवं उद्योगों पर ब्रिटिश उद्योग व्यापार के विपरीत प्रभाव पड़ने से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई। तत्पश्चात् अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर बड़े उद्योग (Heavy Industries) स्थापित किये। इनमें वस्तुओं का निर्माण मशीनों से किया जाने लगा। स्थानीय बाजार की खपत से अधिक वस्तुएं तैयार की गईं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। मगर अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का दोहन कर जो धन एकत्रित किया उसका निरंतर इंग्लैंड को प्रवाह होता गया।
प्रश्न 10.
धर्म निरपेक्षता क्या होती है? धर्म निरपेक्षता के क्या कारण हैं?
अथवा
धर्मनिरपेक्षीकरण से आप क्या समझते हैं?
अथवा
धर्मनिरपेक्षीकरण के दो कारक लिखें।
अथवा
पंथनिरपेक्षीकरण पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
उत्तर:
धर्म निरपेक्षता का अर्थ (Meaning of Secularism)-भारतीय समाज 20वीं शताब्दी से ही पवित्र समाज (Sacred Society) से एक धर्म निरपेक्ष समाज (Secular Society) में परिवर्तित हो रहा है। इस शताब्दी के अनेक विद्वानों, विचारकों एवं राजनीतिज्ञों ने यह महसूस किया कि धर्म निरपेक्षता के आधार पर ही विभिन्न धर्मों का देश भारत संगठित रह पाया है। धर्म निरपेक्षता के आधार पर राज्य के सभी धार्मिक समूहों व धार्मिक विश्वासों को एक समान माना जाता है।
निरपेक्षता का अर्थ समानता या तटस्थता से है। राज्य सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता है तथा किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्म निरपेक्षता ऐसी नीति या सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत लोगों को किसी विशेष धर्म को मानने या पालन करने के लिये बाध्य नही किया जाता है।
धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ (Meaning of Secularization) धर्म निरपेक्षीकरण को उस सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिनके द्वारा धार्मिक एवं परंपरागत व्यवहारों में धीरे-धीरे तार्किकता या वैज्ञानिकता का समावेश होता जाता है। अनेक विद्वानों ने धर्म निरपेक्षीकरण को अग्रलिखित परिभाषाओं से परिभाषित किया है।
डॉ० एम० एन० श्रीनिवास (Dr. M.N. Srinivas) के शब्दों में “धर्म निरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण शब्द का यह अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, इसका अर्थ विभेदीकरण की प्रक्रिया से भी है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक के एक दूसरे से अधिक पृथक होने से दृष्टिगोचर होती है।”
डॉ० राधा कृष्णन (Dr. Radha Krishnan) के अनुसार, “लौकिकीकरण या धर्म निरपेक्षीकरण, धार्मिक निरपेक्षता व धार्मिक सहअस्तित्ववाद है।” उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर धर्म-निरपेक्षीकरण एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें मानव के व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं, अपितु तार्किक आधार पर की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत धर्म का प्रभाव कम हो जाता है तथा घटनाओं को कार्य-कारण संबंधों के आधार पर समझा जाता है।
आत्मगतता व भावुकता (Subjectivity and Emotionality) का स्थान वस्तु निष्ठता (Objectivity) एवं वैज्ञानिकता ने ले ली है। अतः धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में, धार्मिकता का ह्रास, बुद्धिवाद के महत्त्व, विभेदीकरण, वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता, तथा व्यक्ति को किसी भी धर्म या धार्मिक सोपान की सदस्यता प्राप्त करने की स्वतंत्रता व अधिकार होता है।।
धर्म निरपेक्षीकरण के कारण (Factor of Secularization) धर्म निरपेक्षीकरण से भारतीय समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टिकोणों में काफ़ी परिवर्तन किये गये हैं। इन क्षेत्रों में प्रभाव को देखने से पहले उन कारणों को जानना ज़रूरी है जिन्होंने धर्म निरपेक्षीकरण को संभव बनाया है। धर्म-निरपेक्षीकरण के विकास के निम्नोक्त कारक हैं-
1. धार्मिक संगठनों में कमी (Lack of Religious Organisations)-धार्मिक निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का विकास धार्मिक संगठनों का अभाव कारण रहा है। भारतीय समाज में अनेक धर्मों के संप्रदाय पाए जाते हैं। इन संप्रदायों में हिंदू धर्म ही एक ऐसा संप्रदाय है जिनके अनेक मत पाये जाते हैं। बाकी धर्मों जैसे सिक्ख, ईसाई, मुस्लिम, इन सभी में एक ही मत व संप्रदाय होता है। इसी कारण ये लोग अपने संप्रदाय के प्रति काफ़ी कठोर विचारधारा के होते हैं।
इसके विपरीत हिंदू धर्म में अनेक मतों के कारण कोई अच्छा संगठन नहीं है। एक हिंदू दूसरे हिंदू की धार्मिक आधार पर निंदा या आलोचना करता है। इस सबका प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ा। एक ओर तो लोग उच्च जातियों के अत्याचारों एवं शोषण से दुखी होकर हिंदू धर्म को अपनाया दूसरी ओर पढ़े-लिखे हिंदू इस धार्मिक कट्टरता से दूर होते चले गये। यह लोग हिंदू धर्म में पाये जाने वाले विश्वासों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों, आदर्शों व मूल्य का विरोध कर रहे थे। भारतीय समाज में यह सभी कारण धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में सहयोग देते आ रहे हैं।
2. भारतीय संस्कृति (Indian Culture) भारतीय संस्कृति का अपने आप ही निरपेक्षीकरण हो रहा है क्योंकि भारतवर्ष एक धर्म निरपेक्ष (Secular Republic) गणराज्य है। एक धर्म निरपेक्ष राज्य होने के कारण अनेक धर्मों व जातियों के संप्रदाय एक-दूसरे के नज़दीक आते रहते हैं तथा एक दूसरे संप्रदाय की अच्छाइयां व बुराइयों का भी ज्ञान अर्जित करते रहते हैं तथा उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य संस्कृति ने भी धर्म निरपेक्षीकरण के आधार पर परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाई है।
3. यातायात एवं संचार (Transportation and Communications) यातायात व संचार की सुविधाओं में माज में गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। इन्हीं साधनों की वजह से नये-नये नगरों, व्यवसायों व उद्योगों का भी विकास हुआ। इन विभिन्न साधनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, प्रदेश व देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने से ही आपसी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इससे विभिन्न धर्मों की तार्किक आलोचना की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला। इससे पवित्र-अपवित्र एवं अस्पृश्यता के विचारों में कमी आई। ये सभी तत्त्व धर्म-निरपेक्षीकरण के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
4. पाश्चात्य संस्कृति (Western Culture)-भारतीय संस्कृति के ऊपर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डाला है। यहां के धर्म, कला, साहित्य, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक जीवन में कई परिवर्तनों को पाश्चात्य संस्कृति के संदर्भ में समझा जा सकता है। वास्तव में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के विकास में पाश्चात्य संस्कृति का ही मूल रूप से सहयोग रहा है।
5. आधुनिक शिक्षा (Modern Education)–वर्तमान समय की शिक्षा पद्धति ने भी धर्म-निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के विकास में सर्वोपरि भूमिका निभाई है। भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा पद्धति पाश्चात्य शिक्षा का ही रूप है। शिक्षा पद्धति में पाश्चात्य मूल्यों के विकास के साथ भारतीय मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ। इसका प्रभाव सबसे अधिक धार्मिक विश्वासों व मूल्यों पर पड़ा आधुनिक शिक्षित व्यक्ति केवल मात्र धर्म के आधार पर अंध-विश्वासों, नियमों या बंधनों को नहीं अपनाता।
मूल्यांकन के पश्चात् ही अपने आपको उन बंधनों से बांधता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति ने व्यक्ति की सोच को व्यावहारिकता व वैज्ञानिकता के आधार पर विकसित किया है। इसके साथ ही स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। शिक्षा पद्धति में आये हुए परिवर्तनों के कारण ही भारतीय समाज में लिप्त कई बुराइयों जैसे-छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना, जातीय आधार, उच्च शिक्षा आदि में कमी आई है। सहशिक्षा (Co-education) को भी अवसर दिया जाता है।
6. नगरीयकरण (Urbanization)-नगरीयकरण ने धर्म निरपेक्षीकरण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। शहरों व नगरों में ही धर्म निरपेक्षवाद सबसे अधिक विकसित हुआ। नगरों में ऐसे वह सब साधन मौजूद होते हैं, जैसे विकसित यातायात व संचार की सुविधाएं, उच्च शिक्षा, भौतिकवाद, तार्किकतावाद या विवेकवाद, व्यक्तिवादिता, फैशन, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इत्यादि जो मिलकर धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का विकास करते हैं।
प्रश्न 11.
धर्म निरपेक्षता के भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े?
अथवा
धर्मनिरपेक्षीकरण के भारतीय समाज पर प्रभावों का वर्णन करें।
उत्तर:
भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक, जीवन पर धर्म निरपेक्षता के प्रभाव (Impact of Secularization on Indian Social and Cultural Life)-डॉ० एम० एन० श्रीनिवास ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति Social change in Modern India में धर्म-निरपेक्षीकरण के भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर पड़े अनेक प्रभावों एवं परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का सविस्तार उल्लेख किया जिसका वर्णन अग्रलिखित है-
1. पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा में परिवर्तन (Change in the Concept of Purity and Pollution)-धर्म रण के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा काफ़ी परिवर्तित हई है। इसके प्रभाव के कारण, जाति, व्यवसाय, खान-पान, विवाह, पूजा-अर्चना, संबंधी अनेक धारणाओं में धर्म का प्रभाव कम हुआ है तथा अपवित्रता संबंधी कट्टर विचारों में भी कमी आई है।
विभिन्न जातियों के व्यक्ति आपस में इकट्ठे होकर रेल, बस आदि में यात्रा करते हैं। मिलकर रैस्टोरैंट या रेस्तरां आदि में खाते-पीते हैं। एक जाति दूसरी जाति के व्यवसाय को अपना रही है। निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति के व्यवसायों को अपना रहे हैं जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है।
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के आधार पर भी निम्न जातियों ने उच्च जाति की उच्च जीवन-शैली को अपनाया है। वर्तमान समय में परंपरागत पवित्रता एवं अपवित्रता संबंधी विचारधारा में परिवर्तन हुआ है। अब लोग किसी भी चीज़ को तार्किकता व स्वास्थ्य नियमों के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करने लगे हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि धर्म निरपेक्षीकरण ने भारतीयों की विचारधारा में अनेक आधारों पर परिवर्तन किये।
2. जीवन चक्र एवं संस्कार में परिवर्तन (Change in Life Cycle and Rituals)-संस्कार हिंदू धर्म का मूल आधार माने जाते हैं। भारतीय समाज में मुख्यतः हिंदू धर्म में प्रत्येक कार्य का आरंभ संस्कारों के आधार पर ही होता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जब एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में आता है, तभी ही गर्भदान संस्कार पूरा कर दिया जाता है तथा इसके पश्चात् समय-समय पर दूसरे संस्कार जैसे-चौल, नामकरण, उपनयन (जनेऊ संस्कार), समावर्तन, विवाह आदि किए जाते हैं। जब व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है तो भी अंतिम संस्कार (अंत्येष्टि) किया जाता है अर्थात् हिंदू समाज
की नींव संस्कारों के बीच ही गडी हई है।
वर्तमान समय में बढ़ते धर्म-निरपेक्षीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण इन संस्कारों का संक्षिप्तिकरण हो रहा है। कुछ एक संस्कारों को ही पूरा किया जाता है तथा अन्य संस्कार जैसे-नामकरण, चौथ एवं उपाकर्म इत्यादि को पूरा नहीं किया जाता। ब्राह्मणों एवं उच्च जातियों में विधवा का मुंडन संस्कार किया जाता था जो अब लगभग न के बराबर है। इसके साथ ही कुछ एक संस्कारों को एक साथ ही मिला दिया गया है; जैसे-उपनयन संस्कार विवाह के आरंभ में ही संपन्न करवा दिया जाता है। वर्तमान समय में दैनिक जीवन के कर्मकांड जैसे-स्नान, पूजा, अर्चना, वेद, पाठ, भजन-कीर्तन इत्यादि के लिये भी व्यक्ति नाम मात्र समय देता है। ये सब परिवर्तन बढ़ते धार्मिक निरपेक्षीकरण के कारण ही हैं।
3. परिवार में परिवर्तन (Change in Family) भारतीय समाज में संयुक्त परिवार (Joint family) पारिवारिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण रूप है। सामाजिक जीवन में परिवार एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था माना जाता है। कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण भारतीय समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था को ही उचित व्यवस्था माना जाता था।
परिवार में सभी सदस्य मिलकर साझे रूप से ज़मीन पर खेती करते तथा साझे रूप से ही अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये अपनी आय का खर्च करते थे। संयुक्त परिवार में संपूर्ण पारिवारिक सदस्य सामान्य हित के लिये कार्य करते थे। संयुक्त परिवार में एक साथ तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य इकट्ठे एक ही घर में ही रहते थे।
वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के अनुसार संयुक्त परिवार में भी परिवर्तन हुआ। आज संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। इनकी जगह एकाकी परिवार विकसित हो रहे हैं। संयुक्त परिवारों में जो कार्य पारिवारिक सदस्य मिल-जुल कर एक-दूसरे के सहयोग से पूरा करते थे, आज वही कार्य अनेक दूसरी समितियों व संस्थाओं को हस्तांतरित हो रहे हैं।
वर्तमान समय में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के विचारों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। इसके साथ अब बड़े बूढ़े भी अपनी विचारधारा को नयी पीढ़ी के साथ परिवर्तित कर रहे हैं। परिवारों में जिन त्यौहारों को धार्मिकता के आधार पर परंपरागत रूप से मनाया जाता था। उन त्यौहारों को धार्मिक तथा सामाजिक अवसर अधिक माना जाता है। इन सब आधारों पर स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक संस्था को धर्म निरपेक्षीकरण ने पूर्णतः प्रभावित किया है।
4. ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन (Change in Rural Community)-धर्म निरपेक्षीकरण का प्रभाव नगरों के साथ-साथ ग्रामीण समुदाय में भी देखने को मिलता है। ग्रामीण समुदायों में जातीय पंचायतों के स्थान पर निर्वाचित पंचायतों का विकास हो रहा है। जहां पर भी ये जातीय पंचायतें अगर हैं भी तो वहां पर ये धार्मिक लक्ष्यों के आधार पर नहीं बल्कि राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर संगठित की गई हैं।
ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान जातीय या धार्मिकता के आधार पर होता था, वहां अब धन व संपत्ति के आधार पर होने लगा है। वर्तमान समय में निम्न जातियों के व्यक्तियों को भी धन के आधार पर उच्च जाति के व्यक्तियों से अधिक सम्मान दिया जाने लगा है। ग्रामीण समाजों पर परिवार व विवाह संबंधों में भी धर्म निरपेक्षीकरण के परिणामस्वरूप अंतर्विवाह (Intercaste-marriage) का प्रचलन बढ़ा है।
ग्रामों में धार्मिक उत्सव को धार्मिकता के आधार पर कम तथा सामाजिक उत्सवों के रूप में अधिक मनाया जाने लगा है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को मूल रूप से प्रभावित किया है। इस प्रक्रिया ने एक और नये सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में योगदान दिया है तो दूसरी ओर भारतीय प्रथागत अथवा परंपरागत मूल्यों, आदर्शों को भी विघटित करने में अपनी भूमिका निभाई है।

प्रश्न 12.
संस्कृतिकरण क्या होता है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करो।
अथवा
संस्कृतिकरण पर निबंध लिखें।
अथवा
संस्कृतिकरण के अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या करें।
अथवा
संस्कृतिकरण की परिभाषा दें तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
अथवा
संस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए। संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें।
अथवा
संस्कृतिकरण पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
उत्तर:
संस्कृतिकरण का अर्थ (Meaning of Sanskritization)-प्रो० श्रीनिवास ने भारतीय समाज में विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित निश्चित पहलुओं में परिवर्तनों की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण का नाम दिया। उन्होंने, अपनी पुस्तक ‘Social Change in Modern India’ में लिखा है कि भारतीय इतिहास में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है और अब भी यह जारी है।
प्रो० एम० एन० श्रीनिवास ने ‘आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन’ नामक कृति में संस्कृतिकरण के अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, “संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांड, विचारधारा तथा जीवन शैली के उच्च व बहुधा ‘द्विज’ की दिशा में बदल लेता है”
श्रीनिवास उसके आगे लिखते हैं, “साधारण तथा ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् वह जाति स्थानीय समुदाय द्वारा जातीय सोपान में प्रदत्त स्थान से उच्च स्थान का दावा करने लगती है। सामान्यतः ऐसा दावा कुछ समय के पश्चात् बल्कि एक-दो पीढ़ियों के पश्चात् किया जाता है जिसकी उसे स्वीकृति मिल जाती है। कभी-कभी कोई जाति ऐसे स्थान का दावा करती है जिसे मानने के लिए पड़ोसी जाति सहमत नहीं होती है।”
उपरोक्त सत्र दवारा स्पष्ट है कि संस्कतिकरण निम्न जाति, जनजाति एवं अन्य समह की परंपराओं. कर्मकांडों. विचारधारा तथा जीवन शैली में उच्च व्यक्ति व द्विज की दिशा में परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ऐसे परिवर्तनों के कुछ समय के पश्चात उक्त समूह जातीय संस्कृति में प्राप्त पारंपरिक स्थान से उच्च स्थान प्राप्ति का दावा करते हैं।
संस्कृतिकरण की विशेषताएं
(Characteristics of Sanskritization)
1. पदमूलक परिवर्तन (Positional Changes)-संस्कृतिकरण द्वारा निम्न जातियों, जनजातियों में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं। इस संबंध में श्रीनिवास लिखते हैं, “संस्कृतिकरण से व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होते हैं। इसके कारण संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते। इससे अभिप्राय यह है कि एक जाति अपनी पड़ोसी जाति से ऊपर जाती है व दूसरी नीचे आ जाती है परंतु ऐसा केवल स्थिर सोपानात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही होता है। इससे व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है।”
2. संस्कृतिकरण केवल ब्राह्मणीकरण नहीं है। (Sanskritization is not Merely Brahmani-zation) श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों में यह पाया कि ‘कुर्ग’ ब्राह्मणों की जीवन पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं। मगर श्रीनिवास के अतिरिक्त योगेंद्र सिंह ने भी इस बात के माना है कि संस्कृतिकरण केवल ब्राह्मणीकरण नहीं है। यह ब्राह्मणीकरण से वृहद् अवधारणा है जिसमें क्षत्रियकरण तथा वैश्यकरण भी सम्मिलित है। क्योंकि निम्न जातियां क्षत्रियों व वैश्य की परंपराओं व विचारधाराओं का भी अनुसरण करती हैं।
3. संस्कृतिकरण के कई प्रारूप हैं (Sanskritization has many Models)-संस्कृतिकरण का वर्ण ही केवल एक प्रारूप नहीं है, कई प्रारूप हैं। मिल्टन सिंगर (Milton Singer) ने कहा है, “संस्कृतिकरण के एक या दो नहीं बल्कि कम से कम तीन या चार आदर्श मौजूद हैं।”
4. उच्च जातियों का अनुकरण (Imitation of High Castes) निम्न जातियां, जनजातियां तथा अन्य समूह हिंदू जातियों की परंपराओं, लोक रीतियों, विचारधाराओं एवं व्यवहार के तरीकों को अपनाती हैं। वे द्विजों द्वारा किए जाने वाले कर्मकांडों को करती हैं। यद्यपि जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जातियों को ऐसा करने की मनाही है। संस्कृति निम्न वर्गों द्वारा उच्च जातियों की जीवन शैली के अनुकरण की प्रक्रिया है।
संतिकरण का संबंध समह से है (Sanskritization is Related to Group)-संस्कतिकरण के दवारा समूह की स्थिति में परिवर्तन आता है। यह अकेले व्यक्ति व परिवार से संबंधित नहीं है क्योंकि यदि व्यक्ति संस्कृतिकरण द्वारा उच्च जातीय स्थिति का दावा करने लगे तो संभव है कि उसे अपनी जाति के अन्य सदस्यों के विरोध, हास्य व व्यंग्य, निंदा व चर्चा कर सामना करना पड़े।
6. निरंतर प्रक्रिया (Continuous Process)-संस्कृतिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जो अविरुद्ध जारी रहती है। श्रीनिवास का मानना है कि केवल दक्षिण भारत के वर्गों में ही संस्कृतिकरण नहीं पाया जाता बल्कि देश को विभिन्न भागों, ग्रामीण, जनजातीय तथा नगरीय समुदाय में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है।
7. गैर-हिंदुओं का भी संस्कृतिकरण होता है (There is also Sanskritization of Non-Hindu) केवल हिंदू जातियों का ही नहीं बल्कि गैर-हिंदू जातियों का भी संस्कृतिकरण होता है। भारत की जनजातियों; जैसे भील, गोंड, औगज आदि का संस्कृतिकरण हुआ। उसके बाद वह हिंदू कहलाईं।
8. संस्कृतिकरण विरोध रहित नहीं है (Sanskritization is not without Opposition)-संस्कृतिकरण विरोध रहित नहीं है, जब निम्न जाति पूर्व प्राप्त सामाजिक स्थिति से उच्च स्थिति का दावा करती है तब उच्च जातियों द्वारा उसका विरोध होता है। क्योंकि निम्न जातियों के ऐसा करने से उनका स्थान पड़ोसी जाति से ऊपर (उच्च) हो जाता है। फलस्वरूप पड़ोसी उच्च जाति की कथित जाति से सामाजिक दूरी तो घटती ही है बल्कि उसका अपना स्थान पहले से निम्न हो जाता है। श्रीनिवास का मानना है कि उत्तरी बिहार में जब राजपूतों और ब्राह्मणों ने अहीरों को विजों के प्रतीक चिन्हों को अपनाने से रोका तो उनके बीच संघर्ष आरंभ हो गया।
निम्न वर्गों में सामाजिक परिवर्तन (Social Changes Among Lower Classes)-संस्कृतिकरण निम्न वर्गों, निम्न जातियों, जनजातियों तथा ऐसे अन्य समूहों में सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत निम्न जातियों की लोक रीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं, प्रथाओं, मूल्यों, शिष्टाचारों, विश्वासों, कर्मकांडों तथा मान्यताओं में परिवर्तन आता है।
10. उच्चतर स्थिति का दावा (Claim of Higher Status)-संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जातियां तथा जनजातियां, जातीय सोपान में उन्हें जो स्थान प्राप्त होता है, उससे उच्च स्थान होने का दावा करती हैं। श्रीनिवास लिखते हैं. “हमें भारत की 1921 की जनगणना रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर भारत के अहीरों ने उपनयन डालकर क्षत्रिय कहलाना आरंभ कर दिया।”
प्रश्न 13.
संस्कृतिकरण के निम्न जातियों पर क्या प्रभाव पड़े?
उत्तर:
भारतीय समाज में संस्कृतिकरण से जाति व्यवस्था पर कई प्रभाव पड़े। इस प्रक्रिया के चलते जाति एवं वर्ग नहीं रह पाया विशेषतः निम्न जातियों में अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास जारी हैं। इससे उनके पारंपरिक जातीय प्रतिबंध शिथिल होते हैं। संस्कृतिकरण से निम्न जातियों पर पड़ने वाले प्रभावों व इससे निम्न जातियों में होने वाले परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है
(1) संस्कृतिकरण से निम्न जातियों में गतिशीलता बढ़ी।
(2) संस्कृतिकरण से निम्न जातियों की प्रस्थिति में सुधार हुआ है। उच्च जातियों की परंपराओं, कर्मकांडों, विचारधारा व जीवन शैली को अपनाने के कुछ समय के पश्चात् निम्न जातीय समूह अपने से तुरंत ऊपर जाति से उच्च स्थान होने का दावा करने लगी हैं। जब वे स्थानीय जातीय सोपान (Local Caste Hierarchy) में वांच्छित स्थान ग्रहण कर लेती हैं तो उससे उनमें पदमूलक सुधार (Positional) होता है।
(3) संस्कृतिकरण से निम्न जातियों की व्यावसायिक स्थिति में परिवर्तन आए हैं। उन्होंने अशुद्ध एवं अपवित्र समझे जाने वाले अपने पारंपरिक व्यवसाय छोड़ने प्रारंभ किए तथा शुद्ध व्यवसायों को अपनाया। यद्यपि पवित्र व्यवसायों को अपनाने की उनको मनाही है मगर पवित्रता के प्रति उनकी बढ़ती चेतना के कारण उन्होंने उच्च कहे जाने वाले व्यवसायों को अपनाना प्रारंभ किया है।
(4) संस्कृतिकरण से उनकी संस्कृति-लोक रीतियां, परंपराएं, प्रथाएं, विश्वास, मूल्य, व्यवहार व शिष्टाचार के तरीकों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना प्रारंभ किया जिससे उनकी जीवन पद्धति प्रभावित हुई।
(5) संस्कृतिकरण से निम्न जातियों के धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाना प्रारंभ किया है। यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ करना प्रारंभ किया हैं। अशुद्धता का परित्याग तथा शुद्ध कार्यों को अपनाया है। हिंदू त्योहारों को मानने लगे हैं।
(6) उनकी आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उद्योगों में व सरकारी नौकरियों में उनके प्रवेश से उनकी आय में वृद्धि हुई। वह शैक्षणिक, तकनीकी व व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्यरत होने लगे। आधुनिक व्यवसायों से उनकी आय बढ़ी जिससे उनकी आर्थिक स्थित में सुधार हुआ।
(7) निम्न जातियों के सामाजिक जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जातीय प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए इनके सदस्यों ने शिक्षा प्राप्त करनी प्रारंभ की है। उद्योगों, कार्यालयों व प्रशासन में नौकरियां प्राप्त की हैं। इससे उनकी समाज के उच्च वर्गों से अंतःक्रिया होने लगी। फलस्वरूप जातीय सामाजिक दूरी में कमी आई।
(8) आर्थिक स्थिति में सुधार, शिक्षा ग्रहण करने, नगरों के लिए स्थानांतरण व आवागमन और संचार साधनों के उपयोग से निम्न जातियों के रहन-सहन में परिवर्तन आया। उन्होंने पक्के भवन बनाने आरंभ किए। घर में फर्नीचर, मेज-कुर्सियां, दीवान, टी०वी०, फ्रिज, पंखे, रसोई-गैस आदि सुख-सुविधा की प्रत्येक वस्तु रखना प्रारंभ की।
(9) संस्कृतिकरण से निम्न जातियों के अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़े हैं। उनमें गतिशीलता के बढ़ने, पवित्र व्यवसायों को अपनाने, उच्च शिक्षा ग्रहण करने, धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करने से हीनता की भावना (Inferiority Complex) में कमी आई।
प्रश्न 14.
पश्चिमीकरण क्या होता है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करो।
अथवा
पाश्चात्यकरण की चार विशेषताएँ बताएँ।
अथवा
पश्चिमीकरण का अर्थ बताएँ तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
अथवा
पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्वों एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
अथवा
पश्चिमीकरण की कोई तीन विशेषताएँ लिखें।
अथवा
पश्चिमीकरण को परिभाषित करें।
उत्तर:
पश्चिमीकरण का अर्थ (Meaning of Westernization) आम तौर पर पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों के भारत पर प्रभाव से लिया जाता है। पश्चिमी देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी व अमेरिका ऐसे राष्ट्र हैं जिनका भारतीय समाज पर काफ़ी प्रभाव रहा है। भारत में विशेषतयः शिक्षित वर्ग इन देशों के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करते रहे हैं। प्रो० एम० एन० श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की बहुपक्षीय विवेचना की है।
अन्य समाजशात्रियों ने भी अत्र-कुत्र पश्चिमीकरण के अर्थ की व्याख्या की है हालांकि अधिकांश विद्वानों ने अपना ध्यान भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों की व्याख्या करने पर केंद्रित किया है। एम० एन० श्रीनिवास ने अपनी कृति ‘आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन’ में लिखा है, “पश्चिमीकरण शब्द के मैंने ब्रिटिश के डेढ़ सौ से अधिक वर्ष के शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है और यह शब्द विभिन्न स्तरों संस्थाओं, प्रौद्योगिकी, विचारधाराओं व मूल्यों आदि में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है।”
श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के अंतर्गत केवल ब्रिटिश शासन या इंग्लैंड के भारत पर प्रभावों को ही सम्मिलित किया है।
पश्चिमीकरण की विशेषताएं
(Characteristics of Westernization)
1. स्वतंत्रता उपरांत जारी (Continue After Independence)-पश्चिमीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजों के भारत से चले जाने के साथ समाप्त नहीं हुई। मगर यह देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी निरंतर जारी है। भार के लगातार बढ़ते प्रचार-प्रसार, ब्रिटिश की तरह खाने-पीने की आदतों, शिष्टाचारों (चरण-स्पर्श के स्थान पर गुड मार्निंग, गुड-इवनिंग, स्वीट ड्रीमज़ आदि अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना) विचारधाराओं (भारतीय राष्ट्रपति का ब्रिटिश रानी की तरह संवैधानिक मुखिया होना तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियों का होना) से पता चलता है कि भारत का वर्तमान समय में भी पश्चिमीकरण हो रहा है।
2. पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण से भिन्न है (Westernization is Different from Modernization) यद्यपि पश्चिमीकरण से आधुनिकीकरण की बढ़ावा मिलता है परंतु यह दोनों एक-दूसरे से भिन्न धारणाएं है। पश्चिमीकरण का संबंध ब्रिटिश संपर्क में आने के पश्चात् भारत समाज पर पड़ने वाले अच्छे-बुरे सभी प्रकार के प्रभावों से है जबकि आधुनिकीकरण के अंतर्गत पश्चिमी देशों इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस व अमेरिकी गैर-पश्चिमी राष्ट्रों जापान एवं चीन आदि के भारत पर सकारात्मक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रभाव तथा भारत में ज्ञान-विज्ञान तथा भारत में ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीक के विकास के कारण हुए परिवर्तन का भी आधुनिकीकरण कहा जाता है।
3. ब्रिटिश संस्कृति का भारतीय समाज पर प्रभाव (Impact of British Culture on Indian Society) पश्चिमीकरण भारतीय समाज पर ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव है। यद्यपि भारत पर अनेक अन्य पश्चिमी समाजों का काफ़ी प्रभाव रहा है मगर पश्चिमीकरण के अंतर्गत अन्य पश्चिमी देशों की संस्कृतियों का प्रभाव सम्मिलित नहीं है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए श्रीनिवास ने कहा है, “पश्चिमीकरण शब्द की मैंने ब्रिटिश के डेढ़ सौ से अधिक वर्ष के शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है।”
4. पश्चिमीकरण शहरी लोगों तक ही सीमित नहीं है। (Westernization is not Confined to Urbanites) ब्रिटिश काल के दौरान पश्चिमीकरण के प्रभाव उन शहरी लोगों या बड़े नगरों तक सीमित नहीं थे जिनके संपर्क में अंग्रेज़ आये बल्कि हज़ारों ग्रामीण श्रमिक, छोटे कर्मचारी सैनिकों के रूप में अंग्रेजों के संपर्क में आये तथा जिससे सुदूर स्थित गांवों का पश्चिमीकरण हुआ।
5. जटिल प्रक्रिया (Complex Process)-पश्चिमीकरण काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, समुदायों, वर्गों तथा समूहों पर पश्चिमीकरण के एक जैसे प्रभाव नहीं पड़े। सुशिक्षित ब्रिटिश प्रशासन, सेनाओं में कार्यरत तथा शहरी लोग अशिक्षित तथा ग्रामीणों से अधिक पश्चिमीकृत हो गये। जैन धर्म के अनुयायी अधिक तथा मुसलमान कम पश्चिमीकृत हुए।
श्रीनिवास ने अपनी कृति ‘आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन’ में लिखा है “पश्चिमीकरण का स्वरूप व गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न रही है। कुछ लोगों की वेषभूषा, भोजन के तरीके, भाषा, खेलकूद तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं पश्चिमीकृत हो गईं जबकि अन्य समूहों ने पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, कलाओं तथा साहित्य को अपना लिया।”
6. चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया (Conscious and Unconscious Process)-पश्चिमीकरण चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया है। संस्कृति के कुछ पहलुओं जैसे-भाषा व तकनीक इत्यादि को सोच-समझा कर भारतवर्ष में लागू किया गया। भारतीयों द्वारा चेतन रूप में इन्हें अपनाया गया। मगर पश्चिमीकरण के तरीकों, मूल्यों, शिष्टाचारों, खान-पान की आदतों तथा विश्वासों को अचेतन रूप में भारतीयों ने ग्रहण किया। चरण स्पर्श के स्थान पर हाथ मिलाकर तथा गुड मार्निंग करके अभिवादन करना, भूमि पर आसन बिछा कर हाथ से भोजन ग्रहण करने के स्थान पर कुर्सी-मेज पर चम्मच से खाना-खाना इसके उदाहरण हैं।
7. नैतिक रूप से तटस्थ (Ethically Neutral)—पश्चिमीकरण द्वारा भारतीय समाज में कई प्रकार के अच्छे व बुरे, नकारात्मक एवं सकारात्मक तथा संगठनात्मक एवं विघटनात्मक परिवर्तन आये। पश्चिमीकरण का संबंध परिवर्तनों के सकारात्मक व नकारात्मक पहलओं से नहीं है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अर्थात पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ है।
8. इसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव सम्मिलित (It Includes Direct and Indirects Impacts) ब्रिटिश के भारत पर शासन के दौरान अंग्रेज़ों का सहस्त्रों भारतीयों से प्रत्यक्ष संपर्क हुआ। लेकिन करोड़ों ऐसे भारतीय भी हैं जिनके साथ कभी भी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ। फिर भी उन पर काफ़ी ब्रिटिश प्रभाव पड़ा।
कई लोग ब्रिटिश काल में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। अंग्रेजों के संपर्क में उन पर कई प्रभाव पड़े। इन लोगों ने ब्रिटिश संस्कृति का अपने पारिवारिक सदस्यों में बीजारोपण किया। ऐसे परिवारों से ब्रिटिश संस्कृति उनके संपर्क में आई तथा अन्य लोगों में फैलती गई। अतः पश्चिमीकरण के अंतर्गत ब्रिटिश के भारतीय समाज पर सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव सम्मिलित हैं।
प्रश्न 15.
भारत में आधुनिकीकरण के कौन-से लक्षण देखे जा सकते हैं? उनका विस्तार से वर्णन करो।
उत्तर:
चाहे अंग्रेजों ने भारत में आधुनिकीकरण की नींव रखी थी तथा उसके लिए कुछ प्रयास भी किए थे पर वे इतने काफ़ी नहीं थे कि उन से देश आधुनिक हो जाए। आजादी के पश्चात् सरकार ने देश को विकसित करने की ठानी तथा बहुत से प्रयास किए गए ताकि भारत को भी पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक बनाया जा सके।
आज हमारे सामने कुछ ऐसे लक्ष्ण हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि भारत आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है चाहे वह पूरी तरह आधुनिक नहीं हुआ है। आधुनिकीकरण के इन लक्षणों का वर्णन निम्नलिखित है-
(i) औद्योगीकरण-आज़ादी से पहले हमारे देश में गिनती के ही कुछ उद्योग थे पर आज़ादी के बाद तेज़ी से उद्योग बढ़े हैं क्योंकि उद्योग लगाने के लिए जो हालात चाहिए वे मिल गए थे। चाहे औद्योगीकरण आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है फिर भी यह आधुनिकीकरण के लिए जरूरी है क्योंकि देश में उद्योग लगने से पैसा आएगा, देश का आर्थिक विकास होगा. जनता को रोजगार मिलेगा।
आज भारत में उदयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। दनिया में उदयोगों के मामले में हम काफी पीछे हैं। इस तरह आधुनिकीकरण के लिए पहली शर्त ज्यादा उद्योग की होती है, वह हमारे देश में तेज़ी से अब बढ़ रही है।
(ii) धर्म निरपेक्षता-जब भारत पर राजाओं-महाराजाओं का राज था तो वह किसी एक धर्म को प्रोत्साहित किया करते थे तथा बाकी धर्मों को नफ़रत की दृष्टि से देखा जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद स्थिति बदल गई। उन्होंने किसी भी धर्म को विशेष महत्त्व नहीं दिया क्योंकि वो तो यहां पर पैसा कमाने आए थे।
अंग्रेजों के पश्चात् आज़ादी के बाद भारत सरकार तथा संविधान में भी धर्म निरपेक्षता की नीति अपनायी गई ताकि किसी विशेष धर्म को महत्त्व न मिले तथा सभी धर्मों को बराबर मौका मिले। आजकल के समय में आधुनिकीकरण की यह शर्त है कि देश धर्म होना चाहिए तथा यही नीति भारत में अपनायी गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण की अगली शर्त यानि कि धर्म-निरपेक्षता, हमारा देश पूरी कर रहा है।
(iii) नगरीयकरण-आधुनिकीकरण का अगला लक्षण नगरीयकरण या नगरों का बढ़ना है। हमारे देश पर यह बात लागू होती है। आज से तकरीबन 100 साल पहले हमारी तकरीबन 90% जनसंख्या गांवों में रहती थी पर आज़ादी के पश्चात् इसमें तेजी से कमी आयी। 1991 की जनगणना के अनुसार 25% जनता तथा 2001 की जनगणना के अनुसार 29% जनता शहरों में रहती है।
इसका यह अर्थ हुआ कि जनसंख्या तेजी से गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जा रही है तथा शहरों का तेजी से विकास हो रहा है। अगर हम शहरों के आकार की तरफ देखें तो पिछले दो-तीन दशकों में शहरों के आकार दगने हो गए हैं। इसका अर्थ है कि नगरीयकरण में बढ़ोत्तरी हो रही है। इस तरह हमारा देश आधुनिकीकरण का यह लक्षण भी पूरा करता है।
(iv) शिक्षा-यह कहा जाता है कि जितना ज्यादा कोई देश साक्षर होगा उतना ज्यादा वह आधुनिक होगा क्योंकि शिक्षा का सीधा संबंध आधुनिकता से होता है। अगर हम पश्चिमी देशों की तरफ देखें तो वह आज के समय में आधुनिक माने जाते हैं पर इसके साथ हमें वहां की साक्षरता दर भी देखनी चाहिए। जापान की साक्षरता दर 100%, इंग्लैंड की 99%, रूस की 99.2%, अमरीका की 98% है। इनके अलावा यूरोपीय देशों की साक्षरता-दर काफ़ी ऊँची है क्योंकि ये लोग शिक्षा पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं।
ये लोग कुल बजट का 19-20% पैसा शिक्षा पर खर्च करते हैं जबकि हमारा देश सिर्फ 3-3.5% ही खर्च करता है पर अब इसमें धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हो रही है। हमारे देश की साक्षरता दर में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 52% थी जो 2001 में बढ़कर 65% तक पहुँच गई है। इस तरह हम आधुनिकता की यह शर्त भी पूरी करते हैं।
(v) पश्चिमीकरण-अगर हम ध्यान से देखें तो पश्चिमीकरण को ही आधुनिकीकरण मान लिया जाता है। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने 150 सालों से ज्यादा राज किया था तथा यहां पर पश्चिमीकरण की नींव भी उन्होंने रखी थी। उन्होंने ही यहां पर पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत की, पश्चिम की तर्ज पर यहां पर उद्योग लगवाने शुरू किए, यातायात जैसे ट्रेन तथा संचार जैसे तार-डाक इत्यादि की शुरुआत की।
इसके अलावा उन्होंने यहां की शासन पद्धति में भी बदलाव किया तथा इसे भी पश्चिम की तर्ज पर चलाया। आधुनिकीकरण की वजह से जो क्रांति यातायात तथा संचार के साधनों, शिक्षा तथा और कई क्षेत्रों में आयी है, आज़ादी के पश्चात् वह हमारे देश में भी आयी है। हमारे देश में भी पश्चिम की तर्ज पर यातायात, संचार, शिक्षा के साधन विकसित हो गए हैं जिनको देख कर हम कह सकते हैं कि भारत आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है।
(vi) सामाजिक परिवर्तन-आधुनिकीकरण का एक और ज़रूरी लक्षण सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन से मतलब न सिर्फ देखने वाली चीजों में बदलाव बल्कि हमारे सोचने के तरीकों, विचारों में भी परिवर्तन होना चाहिए। यह सब भारत में हो रहा है। भारत के सामाजिक ढाँचे, उसकी संरचना में काफ़ी हद तक परिवर्तन आ गए हैं तथा आ रहे हैं।
यह सब भारत सरकार की कोशिशों का नतीजा है। जाति प्रथा जो हमारे समाज का मुख्य आधार हुआ करती थी अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। इसकी जगह तरह-तरह के वर्ग ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं थीं जो खत्म हो गयी है या हो रही हैं। लोगों के सोचने, रहन-सहन के तरीकों में परिवर्तन आ रहे हैं जो कि आधुनिकता की निशानी है।
(vii) गतिशीलता तथा नए वर्गों का विकास-आधुनिकता की एक और निशानी गतिशीलता भी होती है। गतिशीलता का मतलब होता है एक जगह को छोड़ कर दूसरी जगह जाना तथा यह सब भारत में हो रहा है। लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, अपनी पुरानी नौकरियां छोड़कर नई नौकरियां तलाश कर रहे हैं। यह सब गतिशीलता है।
इस गतिशीलता की वजह से जाति प्रथा में बंधन टूट रहे हैं तथा समाज में नए नए वर्गों का उदय हो रहा है। अब कुछ लोग अगर किसी बात में समानता रखते हैं तो वह एक वर्ग का निर्माण करते हैं चाहे वे किसी भी जाति से हों। इस तरह सामाजिक गतिशीलता तथा नए वर्गों का विकास सामाजिक समृद्धि को बढ़ाता है जोकि आधुनिकीकरण का एक लक्षण है।
प्रश्न 16.
आधुनिकीकरण क्या होता है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करो।
अथवा
आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें।
अथवा
आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
अथवा
आधुनिकता क्या है?
उत्तर:
आधुनिकीकरण का अर्थ (Meaning of Modernization)-आधुनिकीकरण एक वृहद् अवधारणा है। यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अंग्रेजी के शब्द मॉडर्नाइजेशन (Modernization) का हिंदी रूपांतर है जिसका प्रादुर्भाव लैटिन भाषा के मोडो (Modo) शब्द से हुआ। मोडो का अर्थ है प्रचलन अर्थात् जो वस्तु धारणा तकनीक तथा व्यवस्था प्रचलित है, अपेक्षाकृत नवीन एवं श्रेष्ठ है। वह आधुनिक है तथा आधुनिक होने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं।
अर्थात् पारंपरिक में आधुनिकता की और परिवर्तनों की प्रक्रिया आधुनिकीकरण है।” अनेक विद्वानों ने आधुनिकीकरण का अर्थ स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित परिभाषाएं परिभाषित की हैं, आइजनस्टेड (Eisenstadt) ने अपनी कृति आधुनिकीकरण प्रक्रिया एवं परिवर्तन में लिखा है, “आधुनिकीकरण उन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्वरूपों की दिशा में परिवर्तन है, जो सतारहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका में तत्पश्चात् अन्य यूरोपीय देशों में तथा उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में दक्षिण अमरीकी, एशियाई तथा अफ्रीकन देशों में हुए।”
यह परिभाषा आधुनिकीकरण की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से व्याख्या करती है। इसमें 17वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व के विभिन्न देशों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आधुनिकीकरण का नाम दिया है।
दूबे के शब्दों में, “आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा उनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं तथा सामाजिक आदर्श नियमों की ओर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है।” दूबे ने प्रौद्योगीकरण तथा सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों को आधुनिकीकरण कहा है।
आधुनिकीकरण की विशेषताएं / तत्त्व
(Characteristics/Elements of Modernization)
1. नगरीयकरण (Urbanization)-नगरीयकरण आधुनिकीकरण की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मानव समुदाय जनजातीय से ग्रामीण तथा जनजातीय एवं ग्रामीण से नगरीय जीवन की ओर परिवर्तित होता है। समाज में जितना अधिक नगरीयकरण होगा वह उतना ही अधिक आधुनिक कहलाएगा। स्विट्ज़रलैण्ड, अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा फ्रांस आदि आधुनिक समाजों में विकासशील समाजों की अपेक्षा कहीं अधिक आधुनिक समाज नगरीकरण हुआ है।
2. औद्योगीकरण (Industrialization)-औद्योगीकरण का अर्थ है-उद्योगों का विकास। औद्योगीकरण से . समाज में गुणात्मक परिवर्तन आता है। औद्योगीकरण समाज में प्रगति का परिणाम है। इसमें प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है तथा उद्योगों में बड़े पैमानों पर उत्तम गुणवत्ता वाली अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुओं के निर्माण से प्रबल प्रगति को बढ़ावा मिलता है। अतः औद्योगीकरण आधुनिकीकरण का आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
3. धर्म निरपेक्ष शिक्षा (Secular Education) शिक्षा जाति, धर्म व समुदाय, लिंग, रंग तथा जन्म के स्थान के पार पर निर्मित समूहों तक सीमित न होकर सबके लिये उपलब्ध हो। अर्थात् समाज के सभी वर्गों को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर प्राप्त हो उसी को आधुनिकीकरण कहा जा सकता है।
4. शिक्षा का प्रसार (Expansion of Education) शिक्षा के प्रसार से आधुनिकीकरण के द्वार खुलते हैं। किसी भी समाज शिक्षा का जितनी गति से प्रसार व प्रचार होगा उस समाज में उतनी गति से आधनिकीकरण होगा। अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि सब देशों में साक्षरता दर लगभग शतप्रतिशत है। उच्च शिक्षा का भी काफ़ी प्रसार हुआ। फलस्वरूप यह समाज आधुनिकीकृत हो पाए हैं।
5. वैज्ञानिक प्रकृति (Scientific Temper)-वैज्ञानिक प्रकृति से अभिप्राय है मनुष्य में कार्य-कारण के आधार पर घटनाओं को समझने की प्रवृत्ति का विकास। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास आधुनिकीकरण का लक्षण है। इस विकास से व्यक्ति तथ्यों का विश्लेषण तर्क, विवेकशीलता एवं वृद्धि के आधार पर करता है। वह किसी भी चीज़ का अंधानुकरण नहीं करता है। किसी भी समाज में आधुनिकीकरण की गति इस बात से प्रभावित होती है कि वहां पर कितने लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है।
6. संचार एवं यातायात साधनों का विकास (Development of Means of Communication and Transportation) संचार एवं यातायात के साधनों में विकास के कारण लोगों में आपसी संबंध बढ़ते हैं। इससे विभिन्न कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूर्ण किये जाते हैं। औद्योगीकरण को गति मिलती है। संचार एवं यातायात के साधनों के उन्नत का अर्थ है कि संबंधित समाज उन्नत है। वर्तमान समय में मोबाइल, टेलीफोन, ई-मेल (E Mail), फैक्स (Fax) से संचार व्यवस्था में क्रांति आई है तथा बस, रेल व हवाई संपर्क से मानव जीवन में सकारात्मक गुणात्मक (Positive qualitative) परिवर्तन आए हैं।
7. एकाकी परिवारों का विकास (Development of Nuclear Family)-अनेक समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि संयुक्त परिवार परंपरा का तथा एकाकी परिवार आधुनिकता का प्रतीक है। आधुनिकीकरण से एकाकी परिवारों का विकास हो रहा है तथा एकाकी परिवार आधुनिकीकरण को दर्शाते हैं जिसमें पति-पत्नि व अनेक अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। ऐसे परिवारों के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
8. विशिष्ट भूमिकाएं (Specialization Roles)-किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करके विशिष्ट भूमिका अभिनीत करना आधुनिकीकरण का एक तत्त्व है। व्यक्ति द्वारा विशेष शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर वैज्ञानिक, मैनेजर, वकील या अन्य व्यावसायिक (Professional) की भूमिका निभाना व्यक्ति की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
9. शक्ति के निर्जीव स्रोतों का दोहन (Exploitation of Inanimate Sources of Power) लेवी (Levi) ने अपनी कृति ‘Modernization of Structure and Society’ में इस बात पर बल दिया है। शक्ति तथा अधिकाधिक दोहन (Exploitation) आधुनिकीकरण का संकेत चिन्ह है। निर्जीव स्रोतों का दोहन करके उसको समाज की प्रगति के लिये उपयोग आधुनिकीकरण है।
10. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in per Capita Income)-प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आधुनिकीकरण का सूचक है। समाज में कितना आधुनिकीकरण हुआ है। वहां की प्रति व्यक्ति आय से इस बात का अनुमान लगाया जाता है। पश्चिमी समाजों का पूर्वी समाजों से अधिक आधुनिकीकरण हुआ है। पूर्व में भी भारत की अपेक्षा जापान का कहीं अधिक आधुनिकीकरण हआ है।
11. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Co-operation)-भूमंडलीकरण के चलते विश्व का कोई भी समाज अन्य समाजों से अलग नहीं रह सकता। प्रगति, विकास तथा विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य देशों का सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र [United Nation(U.N.)], विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization), विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation), यूनेस्को (Unesco), सार्क (Saarc), नाटो (Nato), आई० एम० एफ० (I.M.F) तथा विश्व बैंक (World Bank) आदि का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आधुनिकीकरण को गति मिलती है।
12. लोकतंत्रीकरण (Democratization)-लोकतंत्रीकरण का अर्थ है लोगों की, लोगों के लिये तथा लोगों के द्वारा सरकार की स्थापना करना। सभी नागरिकों को मौलिकाधिकार प्रदान करना। सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करना, लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना, जीवन में आगे बढ़ने के लिये समान अवसर प्रदान करना इत्यादि। वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर राष्ट्रों में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जो आधुनिकीकरण के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। अब भारतीय लोकतंत्र में परिपक्वता आ रही है।
13. राष्ट्रीयता की भावना का विकास (Development of feeling of Nationality)-जाति, धर्म क्षेत्र, रंग तथा लिंग आदि संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना का विकास आधुनिकीकरण है। ऐसे समाज में स्थानीय निष्ठाओं की अपेक्षा राष्ट्रीयता की भावना को अधिक महत्त्व दिया जाता है।
14. तार्किक नौकरशाही (Rational Bureaucracy)-नौकरशाही किसी भी समाज के प्रशासनिक ढांचे की रीड़ की हड्डी होती है। नौकरशाही के तार्किक होने से प्रशासनिक कुशलता बढ़ती है। यह आधुनिकीकरण का प्रतीक है।
15. लोगों की राजनैतिक भागीदारी में वृद्धि (Increasing Political Participation of the People) लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान तथा उनका राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता अंतः संबंधित है। राजनीतिक गतिविधियों में वोट डालना, विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का ज्ञान रखना, देश के सम्मुख प्रमुख समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करना, सरकार के कार्यों का विशलेषण करना इत्यादि लोगों में क्रियाशीलता से देश के शासन में परिपक्वता, कुशलता तथा जवाबदेही विकसित होती है। इसलिये राजनीतिक जनसहभागिता आधुनिकीकरण का कारक है।
16. पश्चिमीकरण (Westernization)-पश्चिमीकरण भी आधुनिकीकरण का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिसमें मानवतावाद, व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, तर्कवाद, लौकिकीकरण (Secularisation) तथा कर्मवाद पर विशेष बल दिया जाता है। जो समाज पश्चिमीकृत है वह काफ़ी सीमा तक आधुनिक भी है। क्योंकि पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण हुआ है। हालाकि जापान जैसे ही कुछ देशों में पश्चिमीकरण के बिना ही आधुनिकीकरण हुआ है।
प्रश्न 17.
भारत पर आधुनिकीकरण के प्रभावों का वर्णन करो।
अथवा
आधुनिकीकरण के कारण भारत में आए परिवर्तनों का वर्णन करें।
अथवा
आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण से भारतीय समाज में क्या-क्या परिवर्तन हुए? उदाहरण देकर वर्णन कीजिए।
अथवा
भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
उत्तर:
स्वतंत्रता के पश्चात् आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव निम्नलिखित है-
1. शहरीकरण (Urbanization) भारतीय समाज में निरंतर शहरीकरण हो रहा है। सन् 1901 में कुल ख्या के 11% लोग शहरों में रहा करते थे। सन् 2011 की जनसंख्या की गणना के अनुसार शहरों में 32% लोग रहते थे। इसी प्रकार स्वतंत्रोपरांत 1951 में हुई देश में प्रथम जनगणना के अनुसार कल शहर 2844 थे जो कि 1991 में बढ़कर 3696 हो गये।
इसी प्रकार 1951 की गणना के अनुसार देश में 74 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक थी जबकि 1991 में यह संख्या 300 के ऊपर तक चली गई। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। 1901 में केवल एक शहर इस श्रेणी में था, 1951 में यह पांच हो गये। 1991 में 23 नगरों की जनसंख्या 10 लाख या उससे अत्यधिक हो गई। 33% जनसंख्या इन्हीं 23 शहरों में निवास करती है। 25.7 लाख आबादी के साथ मुंबई सबसे बड़ा शहर है।
2. औद्योगीकरण (Industrialization)-स्वतंत्रता के उपरांत भारत में अभूतपूर्व गति से औद्योगीकरण हुआ। उद्योगों का विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। इस अवधि में देश में औद्योगिक क्रांति आ गई। बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। जिसमें उत्पादन घरेलू खपत के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार के लिये किया जाने लगा। जुलाई, 1991 से निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण (Privatization, libralization, Globalization) को विशेष बढ़ावा दिया गया। उद्योगों में पूंजीनिवेश के लिये नियमों का सरलीकरण किया गया। निवेशों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई।
3. पश्चिमीकरण (Westernization)-ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों को पश्चिमीकरण कहते हैं। अंग्रेजों के प्रभावाधीन भारत में सामंतवाद, लौकिकीकरण तथा तर्कवाद का विकास हुआ। देश में नववर्ग का उदय हुआ। यातायात एवं संचार साधनों तथा उद्योगों का विकास हुआ। लोकतंत्रीकरण का विकास हुआ। प्रशासनिक, वैधानिक, न्यायिक ढांचे तथा बैंकिंग, बीमा आदि वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण से आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला।
4. प्रौद्योगिक विकास (Technological Development)-भारत में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। देश में हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेल, टैंक, सुपर कंप्यूटर , प्रक्षेपास्त्र, (Missile), उपग्रहों का विकास भारत में बढती प्रौदयोगिकी का स्वयं ही सिदध प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौदयोगिकी (Space Technology) में तो भारत सुपर पावर (Super Power) बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने तो देश को एक परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया है।
मोबाइल पर अगम्य क्षेत्रों, पहाड़ों, जंगलों से व्यक्ति मोबाइल पर भारत में ही नहीं विश्व के किसी भी क्षेत्र में लोगों से बात कर सकता है। इंटरनैट (Internet) से सूचना क्रांति आ गई है। बायो-प्रौद्योगिकी (Bio-Technology) के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है।
5. लोकतंत्रीकरण (Democratization)-“भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है” धर्म, प्रजाति, जाति व जन्म, स्थान के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी भारतीयों को समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी व्यवसाय को अपनाने, देश के किसी भी भाग में घूमने-फिरने, वयस्क मताधिकार, चुने जाने का सभी नागरिकों को अधिकार है। प्रदेश की सरकारें जनता द्वारा 5 वर्ष के लिये चुनी जाती है।
जो सरकार जनता के हितों की अनदेखी करती है। जनता उसे आगामी चुनावों में वोट न डालकर बदल देती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रैस, संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) तथा चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को सशक्त आधार प्रदान करते हैं। लेकिन देश के लगभग एक तिहाई लोग निरक्षर तथा ग़रीबी रेखा के नीचे होने के कारण विशेषतः ऐसे लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते।
नित नये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गठन के कारण, पुराने दलों में विभाजन के कारण तथा राजनीतिज्ञों की वाक्-पटुता के कारण सांसद् और विधान सभाओं में कई अपराधी जीत कर चुने जाते हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण तथा. अपराध के बढ़ते राजनीतिकरण के कारण भारत की लोकतंत्र की गरिमा को आघात पहुंचता है।
6. शिक्षा का प्रसार (Expansion of Education)-स्वतंत्रोपरांत साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्तरों के लाखों शैक्षिक संस्थान खोले गये। 20वीं शताब्दी विशेषतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सन् 1901 में देश की साक्षरता दर मात्र 5 प्रतिशत थी, जिसमें स्त्रियों एवं पुरुषों में साक्षरता दर क्रमशः 0.60 प्रतिशत तथा 9.83 प्रतिशत थी अर्थात् 500 महिलाओं में से केवल 1 महिला शिक्षित थी।
1951 में देश में साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी लेकिन सन 2011 में जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। पुरुष और महिला में साक्षरता दर लगभग 82% तथा 65% है। केरल, मिज़ोरम, गोआ, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक साक्षर राज्य हैं। बिहार तथा झारखण्ड सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्ष्यद्वीप तथा दिल्ली में सबसे अधिक साक्षर है।
7. आवागमन एवं संचार साधनों का विकास (Development of Transportation and Communication) भारत में स्वतंत्रोपरांत यातायात एवं दूरसंचार के साधनों में काफ़ी विकास हुआ है। देश के कोने-कोने को राष्ट्रीय उच्चमार्गों (National Highways) तथा रेलमार्गों (Railways Lines) से जोड़ा गया है। बसों, रेलों, कारों, टैक्सियों, हवाई जहाजों, नावों तथा समुद्री जहाजों से यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं। डाक एवं तार, दूरभाष, (Telephone) मोबाइल फोन, पेज़र, फैक्स, ई-मेल तथ इंटरनैट इत्यादि संचार माध्यमों से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ है। अतः यातायात एवं संचार साधनों से भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की गति बढी
8. जनभागीदारी में वृद्धि (Increase in People Participation)-स्वतंत्रोपरांत देश में कई लोकसभा तथा अनेक बार राज्यों की विधान-सभाओं, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरपालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। देश की जनता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी भारतीय समाज के आधुनिकीकरण का सूचक है।
9. मानवतावाद (Humanitarianism)-आज़ादी के पश्चात् भारत में मानवतावाद को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (SCs, STs and OBCs) के उत्थानार्थ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गये हैं।
10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास (Development of International Cooperation)-भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निरंतर वदधि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सरक्षा स्थापित करने के उददेश्य से 24 अक्तबर, 1945 को गठित विश्व के सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का भारत मूल सदस्यों में से है। भारत विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा दक्षेस (SAARC) आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है जिसमें वह सक्रिय रूप से भाग लेता है। विश्व के विभिन्न देशों में संघर्षों के समाधान हेतु भी भारत शांति सेनाएं भेजकर महत्पूर्ण योगदान देता है।
11. विशिष्ट भूमिकाएं (Specialized Roles)-विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट भूमिकाएं अभिनीत करने के लिये बल दिया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, या व्यावसायिक पेशेवर (Professionals) अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। विभिन्न विषयों समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इत्यादि के अलग-अलग प्राध्यापक होते हैं। अपने-अपने क्षेत्र में विशेषीकरण (Specialization) प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भूमिका अभिनीत करना आधुनिकीकरण को दर्शाता है।
12. मशीनी सैन्यीकरण (Mechanical Militarization) स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना मुख्यतः पैदल सेना (Marching army) थी। वर्तमान समय में तीनों सेनाओं, थल सेना, वायसेना, जलसेना, (Army, Airforce and Navy) के पास आधुनिकतम हथियार एवं संयंत्र हैं। स्वचालित हथियार टैंक, लड़ाकू जहाज़, मिग 21, 27 व 29 मिराज तथा जगुआर) युद्धपोत, पनडुब्बियां प्रेक्षपास्त्र (अग्नि, पृथवी, त्रिशूल तथा नाग इत्यादि) परमाणु हथियारों तथा अन्य उपकरणों से युक्त भारतीय सेनाएं विश्व की आधुनिक सेनाओं में से एक है। जिनमें लगभग 14 लाख सैनिक देश की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
13. कृषि विकास (Agricultural Development)-भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि का विकास हुआ है। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक खाद्यान्न आपूर्ति के लिये विदेशों से अनाज आयात करता था। मगर उन्नत बीजों (High Yield Variety Seeds) उर्वरकों (Fertilizers) तथा कीटनाशकों (Insecticides) के विकास, वैज्ञानिक कृषि उपकरणों में उपयोग तथा सिंचाई व्यवस्था के विकास के कारण 1960 के दशक के मध्य 1965-66 में देश में हरित क्रांति आई।
खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने, हल के स्थान पर ट्रैक्टरों का प्रयोग आदि से जहां 1950 में देश में लगभग 5 करोड़ टन का उत्पादन होता था। वर्तमान समय में 20 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होने लगा। अब भारत खाद्यान्नों का निर्यात करने लगा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि विकास से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तथा विभिन्न उद्योगों के लिये पर्याप्त सस्ता कच्चा माल मिलने लगा है।
![]()
![]()
![]()