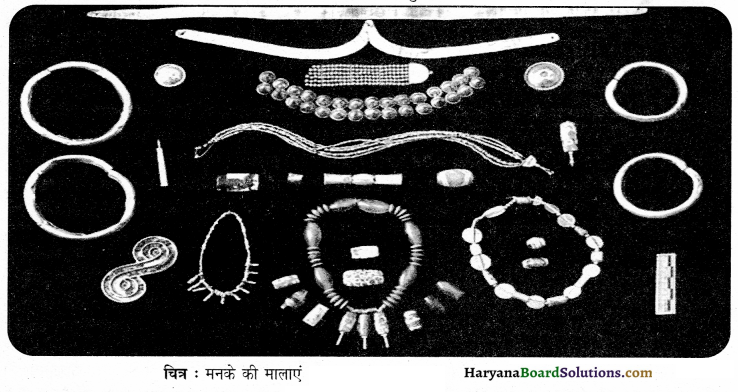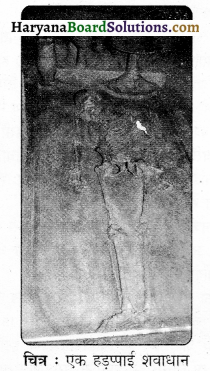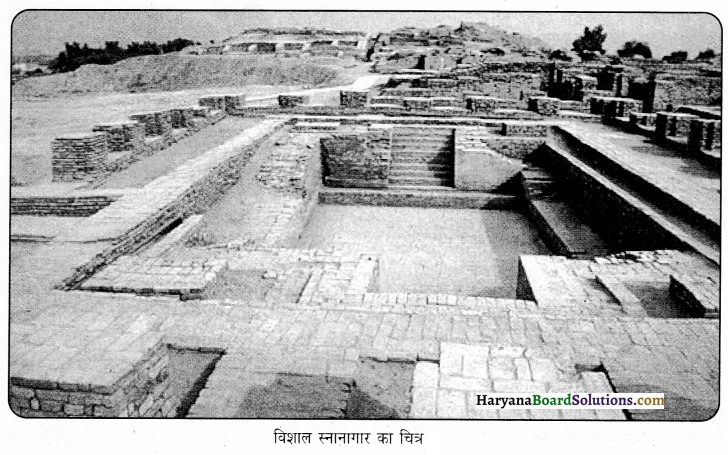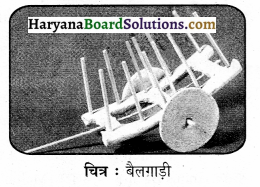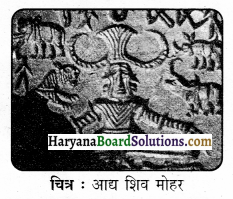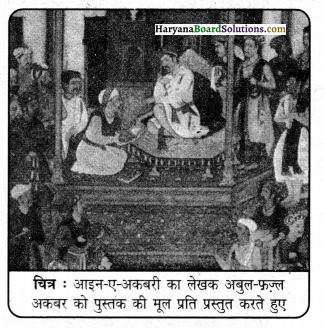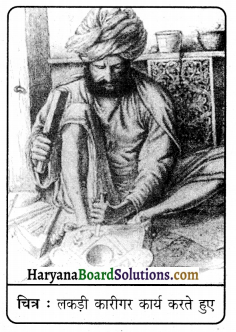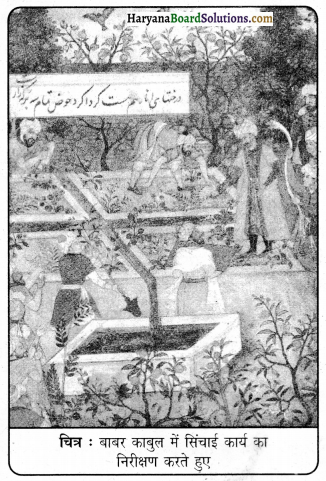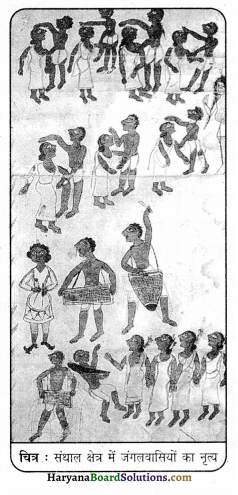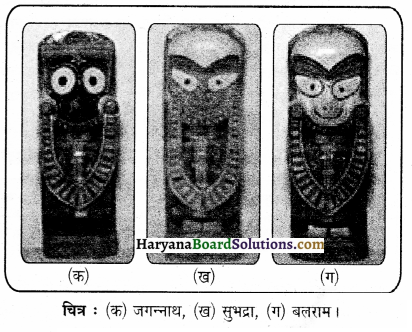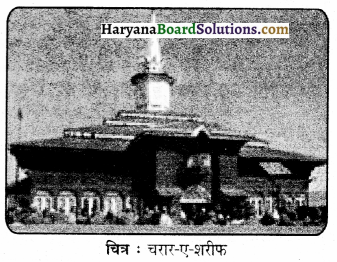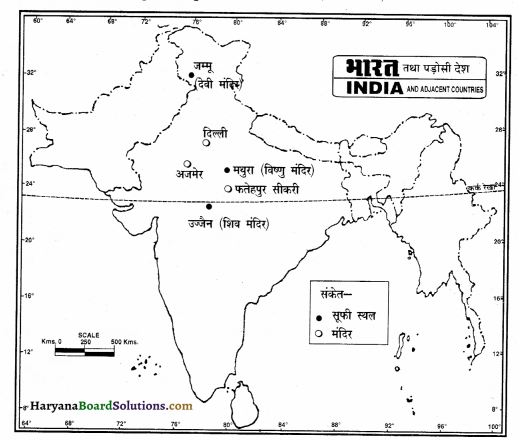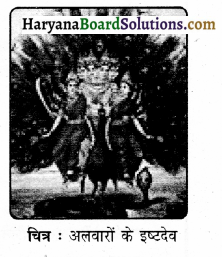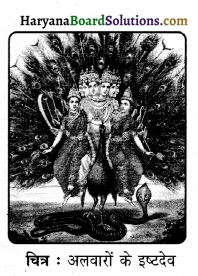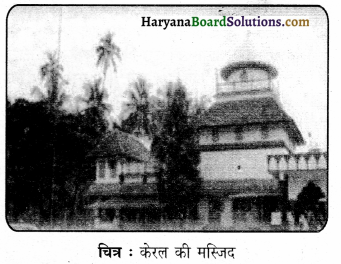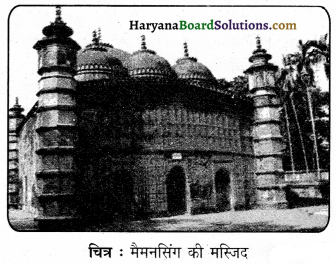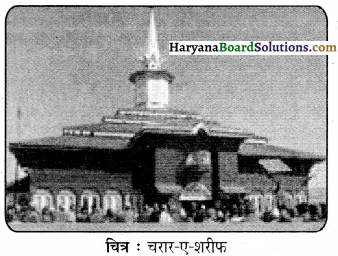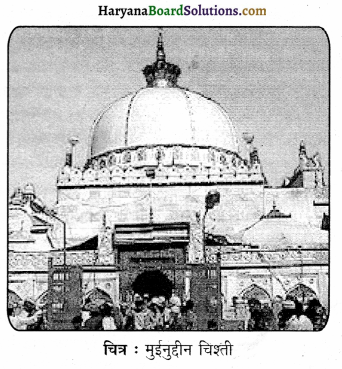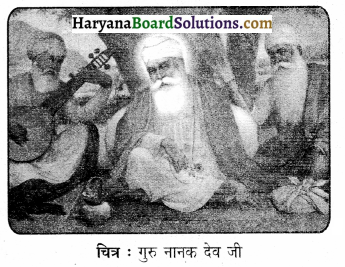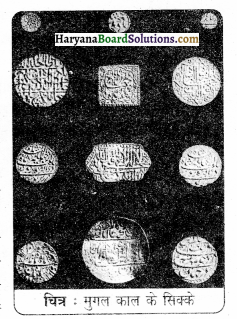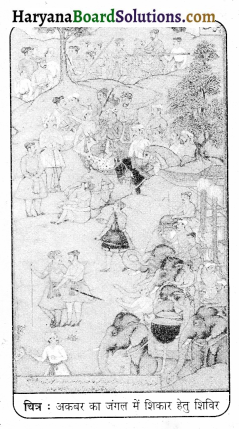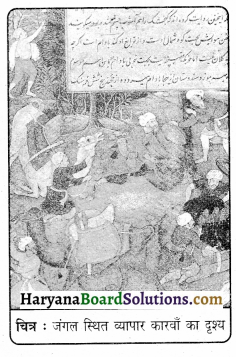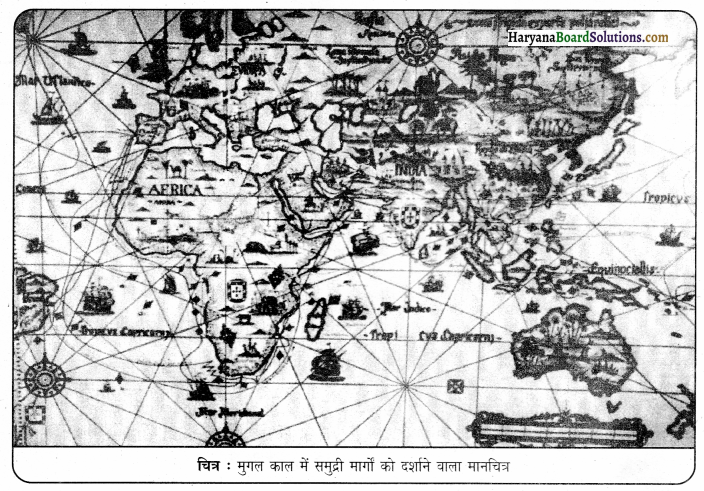HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास
Haryana State Board HBSE 12th Class Geography Important Questions Chapter 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास Important Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class Geography Important Questions Chapter 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
A. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए
1. भारत के आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले योजना किसने बनाई?
(A) जवाहरलाल नेहरू ने
(B) एम०एन० राय ने
(C) एम० विश्वेश्वरैया ने
(D) श्री मन्नारायण अग्रवाल ने
उत्तर:
(C) एम० विश्वेश्वरैया ने
2. गाँधीवादी योजना किसने बनाई?
(A) जवाहरलाल नेहरू ने
(B) एम०एन० राय ने
(C) एम० विश्वेश्वरैया ने
(D) श्री मन्नारायण अग्रवाल ने
उत्तर:
(D) श्री मन्नारायण अग्रवाल ने
3. एम० विश्वेश्वरैया ने दसवर्षीय योजना प्रकाशित की थी-
(A) सन् 1936 में
(B) सन् 1944 में
(C) सन् 1951 में
(D) सन् 1956 में
उत्तर:
(A) सन् 1936 में
![]()
4. योजना आयोग की स्थापना हुई
(A) सन् 1936 में
(B) सन् 1944 में
(C) सन् 1950 में
(D) सन् 1956 में
उत्तर:
(C) सन् 1950 में
5. पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई?
(A) सन् 1936 में
(B) सन् 1944 में
(C) सन् 1951 में
(D) सन् 1956 में
उत्तर:
(C) सन् 1951 में
6. योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ?
(A) जवाहरलाल नेहरू की
(B) एम०एन० राय की
(C) एम० विश्वेश्वरैया की
(D) श्री मन्नारायण अग्रवाल की
उत्तर:
(A) जवाहरलाल नेहरू की
7. पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई?
(A) उद्योग को
(B) कृषि को
(C) गरीबी हटाने को
(D) रोजगार को
उत्तर:
(B) कृषि को
8. गरीबी हटाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य था?
(A) दूसरी
(B) चौथी
(C) पाँचवीं
(D) छठी
उत्तर:
(C) पाँचवीं
9. गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस योजना के दौरान लागू किया गया?
(A) दूसरी
(B) तीसरी
(C) चौथी
(D) पाँचवीं
उत्तर:
(B) तीसरी
10. जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई?
(A) पाँचवीं
(B) छठी
(C) सातवीं
(D) आठवीं
उत्तर:
(C) सातवीं
![]()
11. उदारीकरण की नीति के बाद किस योजना का प्रारंभ हुआ?
(A) पाँचवीं
(B) छठी
(C) सातवीं
(D) आठवीं
उत्तर:
(D) आठवीं
12. औद्योगीकरण के विकास पर किस योजना में विशेष ध्यान दिया गया?
(A) पहली
(B) दूसरी
(C) तीसरी
(D) चौथी
उत्तर:
(B) दूसरी
13. किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं?
(A) पहली
(B) दूसरी
(C) तीसरी
(D) चौथी
उत्तर:
(C) तीसरी
14. इंदिरा गाँधी नहर का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ?
(A) 3
(B) 4
(C) 2
(D) 6
उत्तर:
(C) 2
15. भरमौर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन-सी है?
(A) गंगा
(B) यमुना
(C) रावी
(D) ताप्ती
उत्तर:
(C) रावी
16. गद्दी जनजाति किस प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में पाई जाती है?
(A) मणिपुर के
(B) ओडिशा के
(C) हिमाचल प्रदेश के
(D) अरुणाचल प्रदेश के
उत्तर:
(C) हिमाचल प्रदेश के
17. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था?
(A) 1998-2002
(B) 2002-2007
(C) 2007-2012
(D) 2012-2017
उत्तर:
(B) 2002-2007
18. बारहवीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था?
(A) 2007-2012
(B) 2012-2017
(C) 2013-2016
(D) 2009-2014
उत्तर:
(B) 2012-2017
19. विकास एक ……………… संकल्पना है।
(A) द्वि-आयामी
(B) त्रि-आयामी
(C) बहु-आयामी
(D) एक-आयामी
उत्तर:
(C) बहु-आयामी
20. राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया
(A) वर्ष 1938 में
(B) वर्ष 1940 में
(C) वर्ष 1950 में
(D) वर्ष 1952 में
उत्तर:
(A) वर्ष 1938 में
21. …………….. राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे
(A) सरदार पटेल
(B) सरदार मनमोहन सिंह
(C) सरदार मोंटेक सिंह
(D) पं० जवाहरलाल नेहरू
उत्तर:
(D) पं० जवाहरलाल नेहरू
22. बॉम्बे योजना का गठन किया गया
(A) वर्ष 1944 में
(B) वर्ष 1942 में
(C) वर्ष 1945 में
(D) वर्ष 1950 में
उत्तर:
(A) वर्ष 1944 में
23. 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी थीं?
(A) 11
(B) 8
(C) 9
(D) 12
उत्तर:
(D) 12
24. भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ?
(A) वर्ष 1950 में
(B) वर्ष 1951 में
(C) वर्ष 1952 में
(D) वर्ष 1953 में
उत्तर:
(A) वर्ष 1950 में
25. भारत में पहली योजना कब लागू हुई?
(A) वर्ष 1951 में
(B) वर्ष 1952 में
(C) वर्ष 1953 में
(D) वर्ष 1954 में
उत्तर:
(A) वर्ष 1951 में
26. नवगठित नीति आयोग का गठन हुआ
(A) सन् 2015 में
(B) सन् 2014 में
(C) सन् 2013 में
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(A) सन् 2015 में
27. नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया?
(A) जापान में
(B) अमेरिका में
(C) भारत में
(D) सोवियत रूस में
उत्तर:
(D) सोवियत रूस में
![]()
28. योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को मिली-
(A) ब्रिटेन से
(B) अमेरिका से
(C) चीन से
(D) सोवियत रूस से
उत्तर:
(D) सोवियत रूस से
29. विकास का उद्देश्य है-
(A) प्रकृति का दोहन
(B) रोजगार देना
(C) जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
30. सोवियत रूस में कौन-सा विकास का मॉडल अपनाया गया था?
(A) कल्याणकारी मॉडल
(B) समाजवादी मॉडल
(C) मिश्रित मॉडल
(D) पूँजीवादी मॉडल
(B) समाजवादी मॉडल
31. भारत में विकास का कौन-सा मॉडल अपनाया गया है?
(A) समाजवादी मॉडल
(B) मिश्रित मॉडल
(C) पूँजीवादी मॉडल
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(B) मिश्रित मॉडल
32. जनता योजना के जनक थे
(A) मोंटेक सिंह
(B) एम०एन० राय
(C) लास्की
(D) ल्युसियन पाई
उत्तर:
(A) मोंटेक सिंह
33. बंबई प्लॉन को टाटा-बिरला ने कब बनाया?
(A) सन् 1936 में
(B) सन् 1940 में
(C) सन् 1943 में
(D) सन् 1944 में
उत्तर:
(C) सन् 1943 में
34. वह संकल्पना जिसमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान हो, कहलाती है-
(A) विकास
(B) नियोजन
(C) सतत विकास
(D) विकास नियोजन
उत्तर:
(C) सतत विकास
B. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए
प्रश्न 1.
गाँधीवादी योजना किसने बनाई?
उत्तर:
श्री मन्नारायण अग्रवाल ने।
प्रश्न 2.
उदारीकरण की नीति के बाद किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ?
उत्तर:
आठवीं पंचवर्षीय योजना का।
प्रश्न 3.
औद्योगीकरण के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया?
उत्तर:
दूसरी पंचवर्षीय योजना।
प्रश्न 4.
अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं?
उत्तर:
12।
प्रश्न 5.
किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं?
उत्तर:
तीसरी।
प्रश्न 6.
भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है?
उत्तर:
मिश्रित अर्थव्यवस्था।
प्रश्न 7.
अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉर्टी के अनुसार भारत में कौन-सी परियोजना बनाई गई?
उत्तर:
दामोदर नदी घाटी परियोजना।
प्रश्न 8.
वह संकल्पना जिसमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान हो, क्या कहलाती है?
उत्तर:
सतत विकास।
प्रश्न 9.
जन योजना के प्रस्तुतकर्ता कौन थे?
उत्तर:
एम०एन० राय।
![]()
प्रश्न 10.
योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
उत्तर:
सन् 1950 में।
प्रश्न 11.
दसवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई?
उत्तर:
सन् 2002 में।
प्रश्न 12.
योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ?
उत्तर:
जवाहरलाल नेहरू की।
प्रश्न 13.
भरमौर जन-जातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
उत्तर:
हिमाचल प्रदेश में।
प्रश्न 14.
पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई?
उत्तर:
कृषि को।
प्रश्न 15.
जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई?
उत्तर:
सातवीं पंचवर्षीय योजना में।
प्रश्न 16.
निजी क्षेत्र की भूमिका को किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया?
उत्तर:
दसवीं पंचवर्षीय योजना में।
प्रश्न 17.
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?
उत्तर:
सन् 1952 में।
प्रश्न 18.
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई?
उत्तर:
प्रथम पंचवर्षीय योजना के।
प्रश्न 19.
भारत में पंचवर्षीय योजना अथवा नियोजन की शुरुआत कब हुई?
अथवा
पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई?
उत्तर:
1 अप्रैल, 1951 में।
प्रश्न 20.
नियोजन के दो आयाम कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
- खंडीय नियोजन
- प्रादेशिक क्षेत्रीय नियोजन।
प्रश्न 21.
‘निर्धनता का उन्मूलन’ और ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता’ किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे?
उत्तर:
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के।
प्रश्न 22.
पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किसी एक उद्योग का नाम लिखें।
उत्तर:
हथकरघा उद्योग।
प्रश्न 23.
भारत में पर्वतीय क्षेत्र का कितना विस्तार है?
उत्तर:
लगभग 17%।
प्रश्न 24.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ?
उत्तर:
2 फरवरी, 2006 को।
प्रश्न 25.
जनजातीय विकास कार्यक्रम का कोई एक उद्देश्य बताएँ।
उत्तर:
जनजातीय जीवन की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करना।
प्रश्न 26.
‘सतत् विकास’ शब्द का प्रथम बार कब और कहाँ प्रयोग हुआ था?
उत्तर:
सन् 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में।
प्रश्न 27.
सतत् विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया?
उत्तर:
नौवीं पंचवर्षीय योजना में।
प्रश्न 28.
‘द पापुलेशन बम’ पुस्तक किसने लिखी?
उत्तर:
एहरलिच ने।
प्रश्न 29.
‘द लिमिट टू ग्रोथ’ पुस्तक किसने लिखी?
उत्तर:
मीडोस और अन्य ने।
प्रश्न 30.
अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई?
उत्तर:
1 अप्रैल, 2001 को।
प्रश्न 31.
काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई?
उत्तर:
14 नवम्बर, 2004 को।
प्रश्न 32.
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम/मनरेगा कब शुरू हुआ?
उत्तर:
2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश से।
![]()
प्रश्न 33.
निम्नलिखित का पूरा नाम लिखें ITDP, IRDP, NITI, MFDA, SFDA.
उत्तर:
- ITDP : Integrated Tribal Development Programme
- IRDP : Integrated Rural Development Programme
- NITI : National Institute for Transforming India
- MFDA : Marginal Farmers Development Agency
- SFDA : Small Farmers Development Agency
अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
भारत के किन्हीं छः राज्यों के नाम बताइए जहाँ जनजातियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है?
उत्तर:
- मणिपुर
- त्रिपुरा
- असम
- ओडिशा
- छत्तीसगढ़
- झारखण्ड
- सिक्किम।
प्रश्न 2.
पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में किन क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाता है?
उत्तर:
पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी और ग्रामीण उद्योग आदि पर अधिक जोर दिया जाता है।
प्रश्न 3.
स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी?
उत्तर:
स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को गरीबी ने घेर रखा था और भारत विश्व के निम्नतम आय स्तर और प्रति व्यक्ति निम्नतम उपभोग करने वाले राज्यों में से एक था।
प्रश्न 4.
प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था?
उत्तर:
प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास के लिए घरेलू बचत में वृद्धि के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक शासन के स्वरूप से पुनर्जीवित करना था।
प्रश्न 5.
खंडीय नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
खंडीय नियोजन से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों; जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन और संचार सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना।
प्रश्न 6.
क्षेत्रीय नियोजन से आप क्या समझते हैं?
अथवा
प्रादेशिक नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर:
कोई भी देश सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित नहीं हुआ है। अतः विकास के इस असमान प्रतिरूप में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। इस प्रकार के नियोजन को क्षेत्रीय नियोजन भी कहा जाता है।
प्रश्न 7.
भारत में नियोजन का कार्य किसे सौंपा गया है?
उत्तर:
भारत में पहले नियोजन का कार्य योजना आयोग’ करता था परंतु सन् 2016 में भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया और इसी आयोग को नियोजन का कार्य सौंपा गया है।
प्रश्न 8.
नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका अध्यक्ष कौन होता है?
उत्तर:
केंद्र सरकार ने सन् 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
प्रश्न 9.
प्रादेशिक असंतुलन से क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
प्रादेशिक असंतुलन से तात्पर्य प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त विकास की विषमताओं से है। प्रादेशिक स्तर पर देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकासात्मक कार्यों में आगे हैं और कुछ बहुत पीछे हैं।
प्रश्न 10.
भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक आधार प्रदान करना है। इसका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास है।
प्रश्न 11.
विकास का क्या अर्थ है?
उत्तर:
विकास को आधुनिकीकरण का सूचक माना जाता है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी संरचनाओं या संस्थाओं का निर्माण करती है, जो समाज की समस्याओं का समाधान निकालने में समर्थ हो।
प्रश्न 12.
विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर का विकास करना है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों के जीवन का स्तर न केवल ऊँचा हो, बल्कि उन्हें वे सुविधाएँ भी मिलनी चाहिएँ, जिन्हें वे प्राप्त
करके अपने जीवन में सुखी व सम्पन्न बन सकें।
प्रश्न 13.
बॉम्बे योजना क्या थी?
उत्तर:
सन् 1944 में आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक योजना तैयार की जो बॉम्बे योजना (Bombay Plan) के नाम से जानी जाती है। इसमें कहा गया कि आर्थिक विकास के लिए सरकार को बड़े उद्योगों में अधिक पूँजी लगानी चाहिए; जैसे बीमा व्यवस्था, बीमा कंपनियाँ आदि।
प्रश्न 14.
योजना आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था?
उत्तर:
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश का सामाजिक-आर्थिक विकास तेज और सुनियोजित ढंग से करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था।
![]()
प्रश्न 15.
नियोजन के क्या लक्ष्य हैं?
उत्तर:
नियोजन के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
- आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- आर्थिक असमानता या विषमता कम करना।
- लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना।
प्रश्न 16.
लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है?
उत्तर:
आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतलन को रोकने व क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य-क्षेत्र तथा लक्ष्य-समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया है। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रमों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है।
प्रश्न 17.
गरीबी क्या है? इसके प्रकार बताएँ।
उत्तर:
गरीबी से अभिप्राय विकास की कमी, अल्प विकास और पिछड़ेपन से है। प्रतिदिन 2300 कैलोरी से कम वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। प्रकार-
- निरपेक्ष गरीबी
- सापेक्ष गरीबी।
प्रश्न 18.
भारत में गरीबी उन्मूलन रोजगार किन्हीं छः कार्यक्रमों के नाम लिखें।
उत्तर:
- स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक कार्यक्रम (ट्राइसेस)।
- जवाहर रोजगार योजना (JRY)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PAY)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम (मनरेगा)
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
प्रश्न 19.
गहन कृषीय विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया?
उत्तर:
सन् 1966 से सन् 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाएँ चलाई गई थीं। इन वार्षिक योजनाओं में ही गहन कृषीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था।
प्रश्न 20.
नियोजन किसे कहते हैं?
उत्तर:
किसी देश के भविष्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के क्रम को विकसित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है। ये समस्याएँ मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक ही होती हैं जो समय के साथ-साथ बदलती रहती हैं।।
प्रश्न 21.
किसी देश के विकास के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
नियोजन के बिना कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता। वर्तमान युग नियोजन का युग है और नियोजन ही विकास का मूल मंत्र है। किसी देश को गरीबी, भूख, निरक्षरता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करना है तो उसे नियोजन का सहारा लेना पड़ेगा।
प्रश्न 22.
उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ जन-जातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे।
उत्तर:
जन जातीय विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान; जैसे राज्यों के ऐसे क्षेत्रों में आरंभ किए गए थे जहाँ की जनसंख्या 50 प्रतिशत या इससे अधिक जन-जातीय है।
प्रश्न 23.
जन-जातीय विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
उत्तर:
- जन-जातीय और अन्य लोगों के विकास के स्तरों के अंतर को कम करना।
- जन-जातीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
प्रश्न 24.
भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
उत्तर:
राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 29 मार्च, 1992 को स्वीकृति मिलने के पश्चात् आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1992 से लागू की गई। इस योजना में गरीबी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया था। इस योजना पर कुल परिव्यय ₹ 4,95,670 करोड़ था। योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पादन 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि लक्ष्य 5.6 प्रतिशत का था।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
टिकाऊ विकास की संकल्पना का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
टिकाऊ विकास का अर्थ है, वंचित लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी हों और सभी लोगों को बेहतर जीवन बिताने का मौका मिल सके तथा पारितंत्र को कम-से-कम हानि पहुँचे। इस संकल्पना के अनुसार, मनुष्य की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। संसाधनों का उनकी पुनर्भरण की क्षमता के अनुसार उपयोग होना चाहिए ताकि उनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। टिकाऊ विकास में समान हित की भावना जगा पाने की हमारी क्षमता परिलक्षित होनी चाहिए ताकि आय का न्यायपूर्ण वितरण तथा शक्ति और सुविधाओं का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके।
प्रश्न 2.
भारत में टिकाऊ विकास या सतत् विकास की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर:
1960 के दशक के अंत में पश्चिम के विकसित राष्ट्रों में तीव्र औद्योगीकरण के पर्यावरण पर अवांछित परिणाम सामने आने लगे थे। इससे चिंतित लोगों की पर्यावरण संबंधी सामान्य जागरूकता भी बढ़ने लगी। सन् 1968 में प्रकाशित एहरलिच (Ehrlich) की पुस्तक द पापुलेशन बम और सन् 1972 में प्रकाशित भीडोस (Meadows) व अन्यों द्वारा लिखित पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ ने पर्यावरण निम्नीकरण पर लोगों व विशेष रूप से पर्यावरणविदों की चिंता को बढ़ा दिया। इस समस्त घटनाक्रम के संदर्भ में विकास के एक नए मॉडल का विकास हुआ जिसे सतत् पोषणीय विकास कहा गया।
पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने नार्वे के प्रधानमंत्री हरलेम ब्रटलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग का गठन किया। सन् 1987 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘आवर कॉमन फ्यूचर’ के नाम से प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार, “सतत् पोषणीय विकास वह विकास है ज भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना ही वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करें।” समय के साथ यह परिभाषा भी अपर्याप्त मानी जाने लगी, क्योंकि यह वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं को परिभाषित नहीं करती। सन् 1987 के बाद एक और बेहतर तथा अधिक सार्थक परिभाषा सामने आई। श्री कुमार चट्टोपाध्याय के अनुसार, “सतत पोषणीय विकास पारिस्थितिक तंत्र की पोषण क्षमता के अंदर रहकर मानव-जीवन के स्तर को ऊँचा करना है।”
प्रश्न 3.
सतत् पोषणीय विकास के प्रमुख तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
सतत पोषणीय विकास के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं-
- मानव व जीवन के अन्य सभी रूपों का जीवित रहना।
- सभी जीवों, मुख्यतः मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं का पूरा होना।
- जीवों की भौतिक उत्पादकता का अनुरक्षण।
- मनुष्य की आर्थिक क्षमता एवं विकास।
- पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण।
- सामाजिक न्याय और स्वावलंबन।
- आम लोगों की प्रतिभागिता।
- जनसंख्या की वृद्धि दर में स्थिरता।
- जीवन मूल्यों का पालन।
प्रश्न 4.
सन 1966-1969 के दौरान वार्षिक योजनाओं के विशिष्ट लक्षण कौन-कौन से थे?
अथवा
तीन वर्षीय योजनाओं (1966-1969) पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
सन् 1966-1969 के दौरान तीन वार्षिक योजनाएँ बनाई गई थीं। इन योजनाओं में पैकेज कार्यक्रमों को अपनाया गया था। पैकेज कार्यक्रमों के अंतर्गत सुनिश्चित वर्षा और सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ और ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध करवाना था। इसे गहन कृषीय जिला कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। वर्ष 1968-1969 में औद्योगिक उत्पादों में भी वृद्धि होने लगी।
प्रश्न 5.
सखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए।
उत्तर:
सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे-
- इस कार्यक्रम के उद्देश्य के अतंर्गत अभावग्रस्त लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
- सूखा संभावी क्षेत्र में जहाँ अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हों, वहाँ के गाँवों की गरीबी कम करने के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना।
- भूमि और मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकासात्मक कार्य आरंभ करना।
- सूखा प्रवण क्षेत्र के समन्वित विकास पर बल देना।
प्रश्न 6.
जनजातीय विकास परियोजना का वर्णन करें।
उत्तर:
सन् 1974 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ हुई और हिमाचल प्रदेश में भरमौर को पाँच में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला। इस योजना में परिवहन, संचार, कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं को सामाजिक विकास, सामुदायिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस उपयोजना के लागू होने से सामाजिक लाभ में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार, बाल-विवाह में कमी आई है। जनजातीय क्षेत्रों में जलवायु कठोर होती है। संसाधनों की कमी रहती है। आर्थिक-सामाजिक विकास भी नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों का आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और उससे जुड़ी आर्थिक क्रियाएँ जैसे भेड़ व बकरी पालन शामिल है। इन क्षेत्रों में आज भी कृषि परम्परागत तकनीकों से की जाती है।
प्रश्न 7.
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त नोट लिखें।
अथवा
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ-कहाँ पर आरंभ किए गए?
उत्तर:
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पर्वतीय जिले, मिकिड़ व असम उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और तमिलनाडु के नीलगिरी को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों को संरक्षण एवं उनके रख-रखाव के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्य किए गए। इसका मुख्य कार्य वहाँ की वनस्पति एवं कृषि योग्य जमीन का संरक्षण करना था और वहाँ से गए हुए लोगों को उन्हीं के स्थान पर रोजगार प्राप्त करवाना था।
पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए थे
- केवल प्रभावशाली नहीं, सभी लोगों को लाभ मिले
- स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास
- जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश-उन्मुखी बनाना
- अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो
- पिछड़े क्षेत्रों की बाज़ार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुँचाना
- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
प्रश्न 8.
आर्थिक योजना के लिए तीन स्तरीय प्रादेशिक विभाजन का वर्णन करें।
उत्तर:
1. बृहत स्तरीय प्रदेश-ये सबसे उच्च स्तर के प्रदेश होते हैं। इनमें एक से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार के प्रदेश अपनी सीमा के अंदर पूर्ण विकास की क्षमता रखते हैं। ये क्षेत्र भौगोलिक सम्पदा, कच्चे माल, शक्ति के साधनों में आत्मनिर्भर होते हैं।
2. मध्यम स्तरीय प्रदेश यह प्रदेश एक या एक से अधिक राज्यों के कुछ जिलों का संगठित स्वरूप होता है। 3. अल्पार्थक स्तरीय प्रदेश ये सबसे छोटे और निम्न स्तर के योजना प्रदेश होते हैं। इनमें कई विकास केन्द्र शामिल होते हैं।
प्रश्न 9.
भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताओं की तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया में प्रादेशिक विषमताओं की झलक प्रस्तुत होती है। विकास का फल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल पाया जितना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में कुछ उदाहरण उल्लेखनीय हैं जो निम्नलिखित हैं
(1) वर्ष 1999-2000 में बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 6,328 रुपए थी, जबकि दिल्ली में यह आय 35,705 रु० थी। इस प्रकार राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम आय का अनुपात 1:56 था।
(2) देश के विभिन्न भागों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में भी अंतर पाया जाता है। वर्ष 1999-2000 में जम्मू और कश्मीर में गरीबों का प्रतिशत 3.48 था, जबकि ओडिशा में यह 47.95 प्रतिशत था।
(3) नगरीकरण की प्रक्रिया भी विकास का प्रमुख संकेतक माना जाता है। राज्यों में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 5.50 प्रतिशत है, जबकि गोवा में यह 49.77 प्रतिशत है।
प्रश्न 10.
पंचवर्षीय योजनाओं के कोई चार मुख्य उद्देश्य बताएँ।
उत्तर:
पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य चार उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।
- कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार में वृद्धि करना।
- आर्थिक असमानता समाप्त या कम करना।
- आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास में वृद्धि करना।
![]()
प्रश्न 11.
योजना आयोग के कोई चार कार्य बताइए।
उत्तर:
योजना आयोग के कोई चार कार्य निम्नलिखित हैं-
- देश के संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करना।
- योजनाओं की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- आर्थिक विकास में बाधक कारकों का पता लगाना। इन कारकों को ध्यान में रखकर आयोग उन उपायों तथा मशीनरी को भी निश्चित करता है जिनका उपयोग करके आर्थिक विकास की प्राप्ति हो।
प्रश्न 12.
भरमौर क्षेत्र की कोई चार विशेषताएँ बताएँ।
उत्तर:
भरमौर क्षेत्र की चार मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- भरमौर क्षेत्र पर्वतीय होते हैं।
- ये क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं।
- यहाँ की जलवायु कठोर होती है।
- इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है।
प्रश्न 13.
स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भारत में नियोजन (Planning) को क्यों अपनाया गया? अथवा भारत में योजना पद्धति को क्यों चुना गया?
अथवा
नियोजन की आवश्यकता के कोई चार कारण लिखें।
उत्तर:
भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने के मुख्य चार कारण निम्नलिखित हैं
1. पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली-भारत की स्वतंत्रता के समय देश में कृषि की अवस्था बहुत खराब थी, खाने तक के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था। खाद्य वस्तुओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए नियोजन की बहुत आवश्यकता थी।
2. रोज़गार-स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत में बहुत बेरोज़गारी थी। लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए एक ओर तो बड़े उद्योगों को लगाना आवश्यक था और दूसरी ओर लघु-उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता देकर लोगों को रोजगार दिलाना था।
3. औद्योगिकीकरण भारत में उद्योग भी बहुत पिछड़े हुए थे। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उद्योगों को लगाने और पहले से चल रहे उद्योगों में सुधार करने के लिए भी नियोजन आवश्यक था।
4. शिक्षा-उद्योगों के संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारी तथा वित्त प्रशासक मिल सकें, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना आवश्यक था। भारत में छोटे तथा बड़े स्तर पर अनेक संस्थाएँ स्थापित करने की आवश्यकता थी जिससे विद्यार्थी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तथा अन्य व्यवस्था के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकें।
प्रश्न 14.
भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य बताएँ?
अथवा
भारत में नियोजन की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य चार उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि-नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न योजनाओं में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य निश्चित किया गया। जैसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में आठ प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित . किया गया। नियोजन के कारण ही प्रथम पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं योजना तक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लक्ष्यों में तीन गुणा . तक वृद्धि हुई थी।
2. रोजगार के अवसरों में वृद्धि-सभी को रोजगार उपलब्ध कराना नियोजन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक योजना में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने तथा अर्द्धबेरोजगारी को दूर करने के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
3. समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना-नियोजन का उद्देश्य देश में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना है। यह समाज सामाजिक न्याय ( Social Justice) पर आधारित होता है। यह समाज शोषण-रहित सिद्धांत पर आधारित होता है जिसमें लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
4. निर्धनता दूर करना–पाँचवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य ‘गरीबी हटाओ’ था। इसलिए देश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है ताकि गरीब लोगों की आय में वृद्धि हो और उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
प्रश्न 15.
राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं?
उत्तर:
राष्ट्रीय विकास परिषद् के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-
- सभी पंचवर्षीय योजनाओं अथवा वार्षिक योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत (Guidelines) निर्धारित करना।
- योजना आयोग ने योजनाओं का जो प्रारूप तैयार किया है, उस पर विचार-विमर्श करना और उसको अंतिम स्वीकृति प्रदान करना।
- सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा और उसके लक्ष्य निर्धारित करना।
- योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगाह रखना और योजना-अवधि के दौरान हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- लक्ष्य से कम हुई प्रगति के कारणों की समीक्षा करना और ऐसे सुझाव देना अथवा उपाय बतलाना जिनसे कि योजना-लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिले।
प्रश्न 16.
अच्छे नियोजन के लिए आवश्यक चार बातें लिखें।
अथवा
अच्छे नियोजन की चार विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर:
अच्छे नियोजन के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है-
- नियोजन के उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।
- उद्देश्यों को केवल मात्र निर्धारित करने से काम नहीं चलता। इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों तथा उपायों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- नियोजन कठोर नहीं होना चाहिए। इसे इतना लचीला होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन किया जा सके।
- नियोजन के विभिन्न भागों में संतुलन होना आवश्यक है।
प्रश्न 17.
भारत के विकास में पहली एवं दूसरी योजनाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अथवा पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
नियोजन द्वारा विकास का प्रारंभ सर्वप्रथम सोवियत संघ में हुआ और वहाँ पर इसको शानदार सफलता मिली। भारत में नियोजित विकास का सन् 1951 में आरंभ हुआ।
1. पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56)-इस योजना में कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। योजना काल के दौरान कृषि, सामुदायिक विकास तथा सिंचाई कार्यक्रम पर लगभग ₹ 724 करोड़ खर्च किए गए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में कई नए कारखाने लगाए गए; जैसे चितरंजन में रेलवे इंजन बनाने का तथा सिंदरी में खाद बनाने का कारखाना आदि।।
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) इस योजना में समाजवादी समाज की अवधारणा पर बल देते हए सभी वर्गों के विकास पर बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में ₹ 4800 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया था जिसमें से करीब ₹ 4600 करोड़ व्यय किए गए। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था।
प्रश्न 18.
भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
उत्तर:
इस योजना में सघन खेती (Intensive Agriculture), पौध संरक्षण (Plant Conservation) तथा उन्नत बीजों (Improved Seeds) के प्रयोग पर विशेष बल के अतिरिक्त समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर भी विशेष बल दिया गया। इसके साथ ही बड़े उद्योगों तथा खनिजों के विकास के लिए ₹ 3630 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी। इस योजना में आर्थिक विकास दर को 5.7 प्रतिशत के स्तर पर लाना निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे केवल 2.1 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका। इस दौरान 1971 में भारत-पाक युद्ध और इससे पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए लाखों शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
प्रश्न 19.
भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
उत्तर:
नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1997 को लागू की गई और इसकी अवधि 31 मार्च, 2002 तक की थी। इस योजना में प्रस्तावित निवेश ₹ 8,59,200 करोड़ था, जबकि वास्तविक निवेश ₹ 9,41,041 करोड़ रहा। इस योजना के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों पर जोर दिया गया। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ कीमतों को स्थिर रखने, सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, पेयजल तथा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में 6.5 प्रतिशत की प्रस्तावित दर के विपरीत 5.4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जा सकी।
दीर्घ-उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
अथवा
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य सफलताओं का वर्णन करें। अथवा भारत में नियोजित विकास की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
भारत बारह पंचवर्षीय और छः वार्षिक योजनाएँ पूरी कर चुका है। नियोजन के इतने वर्षों में, हमारी उपलब्धियाँ श्रेष्ठ (Outstanding) नहीं रही। फिर भी, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। सन् 1951 की तुलना में (जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई थी) आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है। उपलब्धियों का विश्लेषण योजनाओं के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के सन्दर्भ में किया जाता है। निम्नलिखित तथ्य भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं
1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय आर्थिक संवृद्धि का सूचक है। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि निश्चित रूप से नियोजन योजन के पहले दशक (1950-51 से 1960-61) के बीच राष्ट्रीय आय में 3.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से औसत वृद्धि हुई। दूसरे दशक (1960-61 से 1970-71) में यह घटकर 3 प्रतिशत रह गई। तीसरे दशक (1970-71 से 1980-81) के दौरान यह बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गई। सन् 1980-81 से 2006-07 के बीच यह बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई। दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर बहुत उत्साहवर्द्धक रही। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह 7.8 प्रतिशत तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान यह लगभग 8 प्रतिशत रही। वर्ष 2008-09 के दौरान विश्व मन्दी के कारण वृद्धि दर बहुत कम रही है। फिर भी हमें आशा है कि हम विश्व मन्दी की मार से बचे रहेंगे। हमें 6.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रहने की उम्मीद है जबकि संसार की उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ गतिहीनता की ओर बढ़ रही हैं।
2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि योजनाओं के अधीन आर्थिक विकास को उत्साहित करने वाले तत्त्वों का विकास होने के कारण कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई है तथा रोज़गार सुविधाओं का विस्तार हुआ है। भारत में सम्पूर्ण योजनाकाल में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। सम्पूर्ण नियोजन की अवधि के दौरान, प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। यह इस तथ्य का संकेत है कि विकास की प्रक्रिया पूरी तरह से जड़ पकड़ नहीं पाई है, यद्यपि विकास की गति को अभी उड़ान भरनी है।
3. पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि-पूँजी निर्माण आर्थिक विकास का मूल निर्धारक है। एक देश का आर्थिक विकास पूँजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। पूँजी निर्माण की दर बचत तथा निवेश पर निर्भर करती है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, बचत तथा निवेश की दर में काफी वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 में, भारत में बचत की दर राष्ट्रीय आय का 5.5% थी जो 2010-11 में बढ़कर 32.3% हो गई। 10वीं योजना के अन्त में भारत में निवेश दर का अनुमान 32.5% था, 2010-11 में यह 35.1% अनुमानित है।
4. कृषि का विकास-कृषि विकास के लिए भारत सरकार ने बहुत-सी योजनाएँ चालू की हैं, जिनका कृषि उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज भारतीय कृषि में ऊँची उपज वाले बीज, रासायनिक खाद, मशीनों तथा नए ढंगों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई है, जिसको हरित-क्रान्ति का नाम दिया गया है।
उदाहरणस्वरूप अनाज का उत्पादन 1951-52 में 550 लाख टन से बढ़कर 2011-12 में 2448 लाख टन हो गया था। नियोजन की अवधि के दौरान कृषि उत्पादन की औसत वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। हमने देखा कि कृषि उत्पादन के स्तर में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है किन्तु कृषि उत्पादन की वृद्धि दर इन सभी वर्षों में स्थिर (Stable) नहीं रही। इसमें एक वर्ष से दूसरे वर्ष उतार-चढ़ाव होता रहा है जो कि देश में जलवायु सम्बन्धी संवेदनशीलता का प्रतीक है। उपयुक्त मानसून के कारण अच्छी फसल तथा खराब मानसून के कारण खराब फसल का उत्पादन हुआ है।
5. औद्योगिक विकास योजनाओं के अधीन औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की संख्या, पूँजी निवेश तथा औद्योगिक उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। पूँजीगत वस्तु उद्योग; जैसे लोहा तथा इस्पात, मशीनरी, रासायनिक खादें आदि का बहुत सन्तोषजनक विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश ने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।
उद्योग के पर्याप्त आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के फलस्वरूप आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में दसवीं सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गई है। नियोजन की अवधि (1951-2012) के दौरान औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। अतः योजना के काल में औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (यद्यपि उतार-चढ़ाव से मुक्त नहीं थी) कृषि उत्पादन की वृद्धि दर से काफी अधिक स्थिर रही है।
6. आर्थिक आधारिक संरचना का विकास योजना अवधि में आर्थिक आधारिक संरचना में काफी प्रगति हुई है। इसमें मुख्य रूप से यातायात, संचार के साधन, सिंचाई की सुविधाएँ, बिजली की उत्पादन क्षमता आदि शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में ऊर्जा निर्माण (Power-generation) में बहुत वृद्धि हुई है। सड़कों, रेलवे, बन्दरगाहों, हवाई अड्डों, दूर-संचार, बैंकिंग, बीमा आदि सभी में बहुत विकास हुआ है। योजना अवधि में बेहतर आधारिक संरचना के उपलब्ध होने से आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है। नियोजन काल में नए बिजली-घर स्थापित किए गए हैं। बिजली आपूर्ति में तीव्रता से वृद्धि हुई है।
देश के भिन्न-भिन्न भागों में गाँवों को शहरों के साथ सड़कों तथा रेलों के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिसके कारण देश में कृषि तथा औद्योगिक विकास की तथा श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई है, जिसका लोगों के जीवन-स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। कृषि विकास, नए उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए कर्जे की सुविधाएँ देने के लिए सरकार ने व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है। बैंकों को पिछड़े भागों में शाखाएँ खोलने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसके कारण देश में बैंकों की शाखाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
7. सामाजिक आधारिक संरचना का विकास-सामाजिक आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, परिवार कल्याण आदि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में भी पंचवर्षीय योजनाओं ने बहुत विकास किया है, जैसा कि जीवन की गुणवत्ता से सम्बन्धित आँकड़ों से स्पष्ट होता है
- मृत्यु-दर-सन् 1951 में मृत्यु दर 27 प्रति हजार थी जो कि सन् 2011 में घटकर 7.2 प्रति हजार रह गई।
- औसत आयु-सन् 1951 में 32 वर्ष से बढ़कर 2010-11 में 65.4 वर्ष हो गई।
- शिक्षा सुविधाएँ-स्कूली बच्चों की संख्या सन् 1951 से तीन गुना तथा कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या पाँच गुना बढ़ गई है।
- इंजीनियरिंग कॉलेजों में वार्षिक दाखिलों की संख्या जो सन् 1950 में 7,100 थी अब बढ़कर 1,33,000 हो गई है।
8. रोज़गार योजनाओं की अवधि में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के बहुत प्रयत्न किए गए हैं। प्रथम योजना में 70 लाख, दूसरी योजना में 100 लाख तथा तीसरी योजना में 145 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया। चौथी योजना में 180 लाख लोगों को तथा पाँचवीं योजना में 190 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। सातवीं तथा आठवीं योजनाओं में क्रमशः 340 लाख तथा 398 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। एक अनुमान के अनुसार नौवीं योजना के अन्त तक लगभग 41 करोड़ 64 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 5.8 करोड़ रोज़गार के अवसरों का सजन करने का लक्ष्य था।
9. आधुनिकीकरण-योजनाओं की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक तथा संस्थागत परिवर्तन हुए हैं वे इस बात के सूचक हैं कि अर्थव्यवस्था का काफी आधुनिकीकरण हुआ है। कुछ महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन इस प्रकार हैं-
(i) राष्ट्रीय आय की संरचना में उद्योगों तथा सेवाओं का योगदान काफी बढ़ गया है
(ii) आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने वाले उद्योगों की संख्या
(iii) कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग निरन्तर बढ़ा है। संस्थागत परिवर्तनों में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण सम्मिलित हैं, जो कि विकास की रणनीति, छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर-क्षेत्रीय विस्तार एकाधिकारी व्यवहार पर ‘ प्रतिबन्ध इत्यादि के मुख्य तत्त्व हैं।
10. आत्म-निर्भरता-नियोजन काल में देश में आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में काफी प्रगति देखी जा सकती है। विभिन्न योजनाओं में विदेशी सहायता में निरन्तर कमी हुई है। आयातों की वृद्धि दर भी निरन्तर गिरावट की ओर है। निर्यातों ने खूब उन्नति की है। इनमें निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। अतः भारत में योजनाएँ अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ाने में सफल रही हैं।
संक्षेप में, भारत ने नियोजन की अवधि में विशेष प्रगति की है। देश को औद्योगिक विकास, कृषि के आधुनिकीकरण, व्यापारीकरण एवं सेवा-क्षेत्र के बहुमुखी विस्तार की ओर एक नींव स्थापित करने में सफलता मिली है। किन्तु हमारे नियोजित विकास कार्यक्रमों में गम्भीर दोष भी पाए गए हैं। इन दोषों के कारण ही हमारी उपलब्धियाँ विकास के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकी। काफी कुछ प्राप्त किया जा चुका है, किन्तु बहुत कुछ करना अभी बाकी है, अतः कड़ा प्रयास करना होगा।
प्रश्न 2.
भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य बताइए।
उत्तर:
पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56)-पहली योजना में समग्र विकास पर बल दिया गया था फिर भी मलतः यह एक कृषि प्रधान योजना थी। इस योजना में बिजली को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉर्टी का अनुकरण करते हुए ऐसी अनेक बहुउद्देशीय योजनाओं को आरम्भ किया गया जिनसे बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली-पालन और मृदा अपरदन के नियन्त्रण को बल मिलता था। भाखड़ा नंगल, कोसी, दामोदर व हीराकुड परियोजनाएँ इसके उदाहरण हैं। ग्रामीण समुदायों के विकास के लिए अनेक सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाए गए। उन्हें निवेश, वित्त और सेवाओं के बारे में तथा तकनीकी जानकारियाँ दी गईं।
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)-इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे-
- राष्ट्रीय आय में 25% की वार्षिक वृद्धि।
- आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण।
- रोजगारों के अवसरों को बढ़ाना।
- राष्ट्रीय आय के असमान बंटवारे और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करना।
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्म-निर्भरता का विकास करना था। इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे
- राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि करना तथा निवेश को बढ़ावा देना ताकि विकास की यह दर कायम रह सके।
- खाद्यान्नं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि उत्पादन में इतनी बढ़ोत्तरी करना कि उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।
- आय और सम्पत्ति के वितरण की विषमताओं को कम करना।
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) इस योजना का मुख्य लक्ष्य ‘स्थिरता के साथ विकास’ था। इस योजना के अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे
- विकास की प्रक्रिया को तेज करना।
- कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना।
- विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना।
- अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए औद्योगीकरण।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)-इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना और आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करना। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)-इस योजना के मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी को दूर करना व जनसंख्या के निर्धन वर्ग के जीवन-स्तर में प्रशंसनीय वृद्धि करना।
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-
- अन्न के उत्पादन में वृद्धि।
- सामाजिक न्याय व रोजगार के अवसरों का निर्माण।
- आत्म-निर्भरता तथा बेहतर कुशलता और उत्पादकता।
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) यह योजना नई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना, उद्योग, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि, आयात और निर्यात में भरपूर वृद्धि तथा भुगतान शेष का घटना।
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)-इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-
- सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना और देश को भूख से मुक्ति दिलाना।
- न्यूनतम आवश्यकताएँ; जैसे स्वच्छ जल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ, शिक्षा तथा आवास की सुविधा प्रदान करना।
- सतत् पोषणीय विकास।
- जनसंख्या वृद्धि को रोकना।
- सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।
दसवीं पंचवर्षीय योजना(2002-07) इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-
- आर्थिक विकास की दर को 8% निर्धारित करना।
- औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात और विश्व व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ाने का लक्ष्य रखना।
- अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना।
- सतत् और टिकाऊ विकास के लिए अवसंरचना में वृद्धि करना।।
- वित्तीय और मौद्रिक नीति में अधिक लचीलापन लाना।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना(2007-12)-इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-
- तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास।
- कृषि की विकास दर को दुगुना करना।
- सामाजिक क्षेत्र-शिक्षा तथा स्वास्थ्य का विकास करना।
- ग्रामीण आधारिक संरचना का विकास करना।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना(2012-17)-इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- तीव्र टिकाऊ एवं अधिक समावेशी विकास करना।
- सकल घरेलू उत्पाद की दर 9% निर्धारित करना।
प्रश्न 3.
नियोजन से आप क्या समझते हैं? विकसित योजना का क्या महत्त्व है?
अथवा
नियोजन से क्या अभिप्राय है? भारत में इसकी क्या आवश्यकता है?
अथवा
भारत में आर्थिक नियोजन अपनाने के कारणों का वर्णन करें।
उत्तर:
नियोजन का अर्थ (Meaning of Planning) साधारण शब्दों में, किसी भी देश के सभी साधनों और शक्तियों द्वारा पूर्व निश्चित अवधि के भीतर निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना नियोजन (Planning) कहलाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा देश का इस प्रकार समुचित आर्थिक विकास किया जाता है जिससे उसका लाभ सारे देश को पहुँच सके।
विभिन्न विद्वानों द्वारा नियोजन की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं-
1. भारत के योजना आयोग के अनुसार, “योजना मुख्य रूप से समस्याओं के तर्कशील हल ढूँढने का यत्न है तथा आर्थिक योजना का अर्थ समाज में पाए जाने वाले संभावित साधनों का प्रभावशाली प्रयोग है।”
2. साइमन स्मिथबर्ग तथा थॉमसन के अनुसार, “योजना वह गतिविधि है जिसका संबंध भविष्य के सुझावों के मूल्यांकन तथा उन गतिविधियों से होता है जिनके द्वारा प्रस्तावों को प्राप्त किया जा सके।”
3. टेरी के अनुसार, “वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले तथ्यों, साधनों तथा गतिविधियों का सोच-समझकर चयन, प्रयोग और उन्हें एक-दूसरे के साथ संबद्ध करना ही नियोजन है।”
भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नियोजन की आवश्यकता (Need of Planning for Socio-economic Development in India)-स्वतंत्र भारत के नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। जब रूस में सन् 1917 में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ तो वहाँ भी भारत जैसी विषम आर्थिक परिस्थितियाँ मौजूद थीं और रूस ने इन समस्याओं को नियोजित अर्थव्यवस्था के द्वारा सुलझाया। इसके परिणामस्वरूप उसे देश की आर्थिक उन्नति तथा समृद्धि में आशातीत सफलता मिली। इससे प्रभावित होकर भारत में भी नियोजित अर्थव्यवस्था की योजना बनाई गई। भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
1. पिछड़ी हुई कृषि प्रणाली (Backward Agricultural System)-भारत की स्वतंत्रता के समय देश में कृषि की अवस्था बहुत खराब थी, खाने तक के लिए भी अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था। खाद्य वस्तुओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए नियोजन की बहुत आवश्यकता थी।
2. रोज़गार (Employment)-स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में बहुत बेरोज़गारी थी। लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए एक ओर तो बड़े उद्योगों को लगाना आवश्यक था और दूसरी ओर लघु-उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता देकर लोगों को रोज़गार दिलाना था।
3. औद्योगीकरण (Industrialisation)-भारत में उद्योग भी बहुत पिछड़े हुए थे। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उद्योगों को लगाने और पहले से चल रहे उद्योगों में सुधार करने के लिए भी नियोजन आवश्यक था।
4. शिक्षा (Education)-उद्योगों के संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारी तथा वित्त प्रशासक मिल सकें, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना आवश्यक था। भारत में छोटे तथा बड़े स्तर पर अनेक संस्थाएँ स्थापित करने की आवश्यकता थी जिससे विद्यार्थी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तथा अन्य व्यवस्था के बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकें।
5. आर्थिक संकट में उपयोगी (Useful in Economic Emergency)-भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसने वर्तमान समय में और भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। नियोजन द्वारा ही देश में उपस्थित आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।
![]()
प्रश्न 4.
भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
1 सितंबर, 2001 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की 49वीं बैठक में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को मंजूरी प्रदान की गई। तत्पश्चात् योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 5 अक्तूबर, 2001 को योजना आयोग की पूर्ण बैठक में 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 29 अक्तूबर, 2001 को योजना आयोग के दस्तावेज़ को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2002 को लागू हुई और इसकी अवधि 31 मार्च, 2007 तक रही। दसवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 2001-02 की कीमतों पर ₹ 15,92,300 करोड़ रखा गया जिसमें केंद्रीय योजना का अंश 9,21,291 करोड़ रुपए तथा राज्यों एवं केंद्र-शासित क्षेत्रों का अंश ₹ 6,71,009 करोड़ था। योजना को केंद्र सरकार द्वारा ₹ 7,06,000 करोड़ का बजटीय समर्थन भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे
- इस योजना में निर्धनता अनुपात को सन् 2007 तक 20 प्रतिशत तक तथा 2012 तक 10 प्रतिशत तक लाना था।
- इस योजना के अंतर्गत सन् 2007 तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
- इस योजना में जनसंख्या वृद्धि को भी 2001-2011 के दशक तक 16.2 प्रतिशत तक सीमित रखना था।
- इस योजना में भारत में साक्षरता दर को सन् 2007 तक 72 प्रतिशत तथा 2012 तक 80 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- इस योजना में सन् 2007 तक सभी प्रदूषित नदियों की सफाई का लक्ष्य रखा गया था।
- इस योजना में शिशु मृत्यु दर को सन् 2007 तक 45 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य निश्चित किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था।
इसके अतिरिक्त जिन नीतिगत सुधारों की अपेक्षा योजना आयोग ने 10वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में की थी, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित थे
(i) योजना के लिए सकल बजटीय समर्थन में निरंतर वृद्धि ताकि योजना के अंतिम वर्ष (2006-2007) तक इसे सकल घं उत्पाद के 5 प्रतिशत तक लाया जा सके। इसके लिए इसमें 18.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई थी।
(ii) सरकारी कर्मचारियों की संख्या में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत बिंदु की कटौती। योजना के पाँच वर्षों की अवधि में कोई नई नियुक्ति नहीं।
(iii) सुरक्षा व्यय एवं ब्याज भुगतान को छोड़कर शेष समस्त गैर-योजना व्यय को पाँच वर्षों की अवधि में वास्तविक अर्थों में (In Real Terms) यथावत् बनाए रखना। इसका अर्थ है कि मौद्रिक
रूप में इसमें वृद्धि को 5 प्रतिशत वार्षिक के स्तर तक सीमित रखना था।
(iv) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व (डीज़ल उपकर सहित) को 2001-2002 में 9.16 प्रतिशत से बढ़ाकर 2006-2007 तक 11.7 प्रतिशत करना था। कर राजस्व में वृद्धि को मुख्यतः कराधार में वृद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
(v) सेवा कर के दायरे में व्यापक विस्तार।
(vi) विनिवेश (Disinvestment) में वृद्धियाँ। 10वीं योजना के पहले तीन वर्षों में ₹ 16-17 हजार करोड़ की वार्षिक विनिवेश प्राप्तियाँ।
(vii) राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत तक लाना था।
यद्यपि इस अवधि में आर्थिक विकास की औसत वार्षिक दर 8 प्रतिशत निर्धारित की गई जिसे बाद में घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था। निर्धारित विकास दर को प्राप्त करने के लिए दसवीं योजना में निम्नलिखित चार उपायों पर बल दिया गया था
- ढाँचागत और सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना।
- स्रोतों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।
- देश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- गवर्नेस या सुशासन को बेहतर बनाना।
प्रश्न 5.
भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) का वर्णन करें।
उत्तर:
भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 19 अक्तूबर, 2006 को मंजूरी योजना आयोग द्वारा दी गई। दृष्टिकोण-पत्र में आगामी योजना के निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित थे
(1) विकास दर, आय एवं निर्धनता-
- 9 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करना तथा विकास दर को 2011-12 के अन्त तक बढ़ाकर 10 प्रतिशत के स्तर तक लाना था।
- वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक संवृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना था तथा इसे 10% से 12% के बीच बनाए रखना था।
- उच्च विकास दर के लाभों को व्यापक स्तर पर लाने के लिए कृषि जीडीपी की वार्षिक संवृद्धि दर को 4% तक बढ़ाना।
- रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करना।
- शैक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना।
- अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना।
- उपयोग निर्धनता के हेडकाउंट अनुपात में 10 प्रतिशतांक तक की कमी लाना।
(2) शिक्षा-
- प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर (ड्रॉप आउट रेट) को वर्ष 2003-04 में 52.2% से घटाकर वर्ष 2011-12 तक 20% के स्तर पर लाना था।
- प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जाँच करते रहना।
- 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% करना।
- साक्षरता में लिंग-अंतराल (जेंडर गैप) को 10 प्रतिशतांक तक नीचे लाना।
- प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के अनुपात को वर्तमान में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 15% करना था।
(3) स्वास्थ्य-
- शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर, 30 प्रति दस हज़ार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- कुल प्रजनन दर को 2-1 तक नीचे लाना।
- सन् 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक यह सुनिश्चित करना था कि इसमें कमी न आए।
- 0-3 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में कुपोषण को वर्तमान के स्तर से आधा करना।
- महिलाओं एवं लड़कियों में रक्ताल्पता को ग्यारहवीं योजना के अंत तक 50% तक घटाना था।
(4) महिलाएँ एवं बालिकाएँ-
- 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात को वर्ष 2011-12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016-17 तक 950 करना था।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा कम-से-कम 33 प्रतिशत हो।
- यह सुनिश्चित करना कि काम करने की किसी बाध्यता के बिना सभी बच्चे सुरक्षित बाल्यकाल का आनंद उठाते हैं।
(5) आधारिक अवसंरचना-
- सभी गाँवों एवं निर्धनता रेखा से नीचे के सभी परिवारों में सन् 2009 तक विद्युत् संयोजन सुनिश्चित करना तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक इनमें 24 घंटे विद्युत् आपूर्ति प्रवाहित कराना था।
- सन् 2009 तक 1000 जनसंख्या वाले सभी गाँवों (पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500 जनसंख्या) तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की सड़कें सुनिश्चित करना तथा सन् 2015 तक सभी महत्त्वपूर्ण अधिवासों तक पक्की सड़कें बनवाना था।
- 2007 तक देश के सभी गाँवों तक टेलीफोन पहुँचाना तथा 2012 तक सभी गाँवों में ब्रॉड-बैंड सुविधा मुहैया कराना था।
- सन् 2012 तक सभी को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना तथा सन् 2016-17 तक सभी ग्रामीण निर्धनों को आवास मुहैया कराने के लिए आवास निर्माण की गति में तेजी लाना था।
(6) पर्यावरण-
- वनों एवं पेड़ों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5 प्रतिशतांक की वृद्धि करना।
- वर्ष 2011-12 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्राप्त करना था।
- नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी तरल कचरे को उपचारित करना।
योजना आयोग की स्वीकृति के बाद ग्यारहवीं योजना के इस दृष्टिकोण-पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 9 दिसंबर, 2006 को स्वीकृति प्राप्त हो गई। परिषद् की यह 52वीं बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस 11वीं योजना में कृषि, सिंचाई, जल संसाधनों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया था।\
प्रश्न 6.
भारत की बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) का वर्णन करें।
उत्तर:
भारत की बारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र को प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गई। योजना आयोग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जिन वैकल्पिक लक्ष्यों को पूरा करना था, वे निम्नलिखित थे-
- घरेलू मामलों का निपटारा करना और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारना भी इस योजना का लक्ष्य है।
- 9.0 फीसदी की विकास दर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के साथ है जो हासिल करनी है।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 9.5 फीसदी औसत विकास वृद्धि दर इस योजना का लक्ष्य है।
- इस योजना के तहत कई स्थूल आर्थिक मॉडल के सन्दर्भ में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
- कृषि क्षेत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण त्वरण की आवश्यकता है; जैसे बिजली और पानी की आपूर्ति।
- खनन क्षेत्र में कोयला और प्राकृतिक गैस का अतिरिक्त उत्पादन करना और उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करना।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगारी को दूर करना, बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, सेवा-क्षेत्रों पर आराम की सुविधा का प्रबन्ध करवाना, 10 फीसदी गरीबी कम करने का इरादा है, 2 फीसदी गरीबी अनुमान सालाना योजना अवधि के दौरान एक स्थायी आधार पर कम करना है।
- सन् 2017 तक सभी को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना था तथा सन 2016-17 तक सभी ग्रामीण निर्धनों को आवास मुहैया कराने के लिए आवास-निर्माण की गति में तेजी लाना।
संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि योजना आयोग के द्वारा प्रायः प्रत्येक योजना के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएँ की जाती थीं
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना।
- विदेशी पूँजी पर देश की निर्भरता को कम करना तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना-जो लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं, उनके जीवन-स्तर में सुधार लाना।
- जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना।
- रोज़गार के अवसरों में वृद्धि तथा बेरोज़गारों को रोजगार दिलाना।
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना आयोग देश के भौतिक साधनों और मानवीय संसाधनों (Human Resources) की जाँच करके ऐसी योजनाएँ बनाता है जिससे कि समस्त साधनों का सर्वोत्तम एवं संतुलित उपयोग किया जा सके।