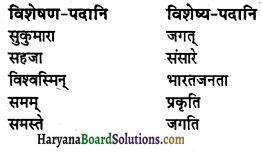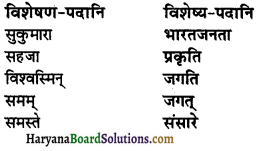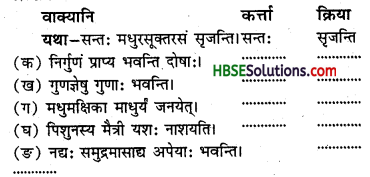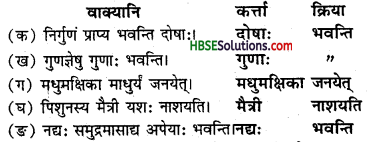Haryana State Board HBSE 11th Class Political Science Important Questions Chapter 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन Important Questions and Answers.
Haryana Board 11th Class Political Science Important Questions Chapter 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन
अति लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन-से दो शब्द जोड़े गए थे? यह संशोधन कब पारित हुआ था ?
उत्तर:
संविधान का 42वां संशोधन सन् 1976 में पारित हुआ। इस द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist) तथा धर्म-निरपेक्ष (Secular) शब्द जोड़े गए थे।
प्रश्न 2.
भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है, व्याख्या करें।
उत्तर:
इसका अर्थ यह है कि भारत अपने आन्तरिक तथा विदेशी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है और यह किसी अन्य विदेशी शक्ति के नियन्त्रण में नहीं है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि अथवा समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत अपनी आन्तरिक तथा बाहरी नीति के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।
प्रश्न 3.
किसी देश के संविधान में अंकित प्रस्तावना का महत्त्व क्यों होता है? कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर:
- प्रस्तावना उस देश के संविधान के संचालन के पथ-प्रदर्शन का कार्य करती है।
- प्रस्तावना संविधान में निहित उद्देश्यों, आदर्शों एवं मूल्यों की ओर संकेत करती है।
प्रश्न 4.
संविधान के दार्शनिक पहलू से क्या तात्पर्य है?
अथवा
संविधान के राजनीतिक दर्शन का क्या अर्थ है?
उत्तर:
संविधान के दार्शनिक पहलू से तात्पर्य संविधान के सार से होता है जो एक देश के सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है।
प्रश्न 5.
किसी देश के संविधान के दर्शन में निहित किन्हीं दो बातों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- संविधान के दर्शन में 3G देश के संविधान के आदर्श एवं सिद्धान्त निहित होते हैं।
- संविधान के दर्शन में 3G देश के संविधान द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ अवधारणाएँ; जैसे न्याय, समानता, विकास एवं स्थिरता आदि निहित होती हैं।
प्रश्न 6.
किसी भी लोकतान्त्रिक देश में संविधान के मूल्य या महत्त्व के कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर:
- संविधान, सरकार पर नियन्त्रण रखने और ‘जन स्वतन्त्रता’ की रक्षा का साधन है।
- संविधान, लोकतन्त्रीय पद्धति के अनुरूप देश में शान्तिपूर्ण तरीके से बदलाव लाने का साधन है।

प्रश्न 7.
भारतीय संविधान के उद्देश्य को संक्षेप में लिखिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान का उद्देश्य है-धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित करना जो भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता और समानता का आश्वासन दे। इसके अतिरिक्त, संविधान भातृत्व को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की अखण्डता को आश्वासन देता है।
प्रश्न 8.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शासन के किन उद्देश्यों की स्पष्टता होती है?
उत्तर:
- न्याय,
- स्वतन्त्रता,
- समानता,
- बन्धुता एवं
- राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता।
प्रश्न 9.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना के कोई दो आधार लिखिए।
उत्तर:
- प्रस्तावना की न्यायिक मान्यता का अभाव होना।
- समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता; जैसे शब्दों की अस्पष्टता का होना।
प्रश्न 10.
भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों के प्रभाव के कारण इसे क्या कहकर आलोचना की जाती है?
उत्तर:
भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों के प्रभाव के कारण इसे ‘उधार ली गई वस्तुओं का थैला’ एवं विविध संविधानों की खिचड़ी’ कहकर आलोचना की जाती है।
प्रश्न 11.
भारतीय संविधान की आलोचना के किन्हीं दो आधारों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर:
- भारतीय संविधान अत्यधिक लम्बा और विस्तृत संविधान है।
- भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनके पीछे कानूनी शक्ति का अभाव है।
प्रश्न 12.
भारतीय संविधान निर्माण पर किन देशों की छाप या प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोई पाँच देशों के नाम लिखिए।
उत्तर:
- इंग्लैण्ड,
- अमेरिका,
- ऑस्ट्रेलिया,
- जापान,
- जर्मनी आदि।
प्रश्न 13.
भारतीय संविधान ‘उधार लिया गया थैला नहीं है। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर:
भारतीय संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों की आँखें मूंद कर नकल नहीं की बल्कि प्रत्येक व्यवस्था को भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान में स्थान दिया जिससे हमारे संविधान में एक मौलिकता आ गई। ऐसे में हमारे संविधान को उधार का थैला कहना गलत है।
प्रश्न 14.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्त्व है?
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बहुत महत्त्व है। संविधान सभा के सदस्य पं० ठाकुरदास भार्गव का कहना है कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य तथा मूल्यवान भाग है। यह संविधान की आत्मा है। इसमें संवैधानिक शक्ति के स्रोत, भारतीय राज्य के स्वरूप, संविधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और संविधान को स्वीकार किए जाने वाली तिथि का वर्णन किया गया है। इसी कारण से कई लोगों द्वारा इसे ‘संविधान की कुंजी’ या ‘संविधान का दर्पण’ कहा जाता है।
लघूत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
भारत एक गणराज्य (Republic) कैसे है?
उत्तर:
गणराज्य का अर्थ यह है कि देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होगा। हमारे देश के मुखिया अर्थात् राष्ट्रपति का पद पैतृक सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। वह एक निश्चित काल (5 वर्ष) के लिए जनता के प्रतिनिधियों (संसद एवं राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा) द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अतः भारत गणराज्य होने की शर्त को पूर्ण करता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो 6 मास के अन्दर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना संविधान के अनुसार आवश्यक है।
प्रश्न 2.
भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य (Secular State) है, व्याख्या करें।
उत्तर:
यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और धर्म के आधार पर राज्य किसी प्रकार के भेदभाव का प्रयोग नहीं करेगा।
सरकार किसी भी धर्म को कोई विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को कोई ऐसा चन्दा या करं देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिससे प्राप्त आय किसी एक धर्म के प्रचार के लिए खर्च की जाने वाली हो । यद्यपि हमारे संविधान में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार का पहले से ही संकेत था, परन्तु अब यह शब्द जोड़ने से संविधान का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया है।
प्रश्न 3.
भारत को समाजवादी (Socialist) राज्य क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इस शब्द का उद्देश्य है कि भारत में इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे समाज के सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछडे लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त हों, मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त हो और आर्थिक विषमता को कम किया जाए। काँग्रेस ने बहुत पहले से ही भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था और उसी दल की सरकार द्वारा यह शब्द संविधान में सन् 1976 (42वें संशोधन द्वारा) में जोड़ दिया गया।
प्रश्न 4.
भारत एक लोकतान्त्रिक (Democratic) राज्य है, स्पष्ट करें।
उत्तर:
भारत एक लोकतान्त्रिक राज्य है जिसमें अन्तिम शक्ति जनता के हाथों में है। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उस कार्यकाल में देश के शासन को चलाते हैं। मन्त्रिमण्डल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात् संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अतः अन्तिम शक्ति जनता में निहित है। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और उनकी रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
प्रश्न 5.
‘प्रस्तावना’ (Preamble) का क्या अर्थ है?
उत्तर:
‘प्रस्तावना’ उस लेख (Document) को कहते हैं जिसे किसी संविधान के आरम्भ होने से पूर्व अंकित किया जाता है। इससे संविधान के मख्य उद्देश्यों, मौलिक सिद्धान्तों तथा उसके आदर्शों का सांकेतिक रूप में वर्णन किया जाता है। प्रस्तावना में उस समाज के सामाजिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक ढाँचे का चित्र देखा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा झरोखा होती है, जिसमें संविधान-निर्माताओं की भावनाओं और आशाओं का दृश्य देखा जा सकता है। यही कारण है कि प्रस्तावना को संविधान-निर्माताओं के ‘हृदय की कुंजी’ और ‘संविधान की आत्मा’ कहा जाता है।
प्रश्न 6.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) लिखें।
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है “हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म-समर्पित करते हैं।

प्रश्न 7.
संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय पर संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर:
न्याय शब्द से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के निजी हित और व्यवहार समाज के सामान्य हितों के अनुकूल हों। इस प्रकार न्याय का उद्देश्य वास्तव में सार्वजनिक भलाई ही है। इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाएँ सम्मिलित हैं। सामाजिक न्याय से भाव यह है कि समाज का सदस्य होने के नाते एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में धर्म, जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने का समान अवसर प्राप्त है और उसे अपने काम की उचित मजदूरी मिलेगी।
राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राजनीति से सम्बन्धित क्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कोई भी पदवी प्राप्त कर सकता है तथा राजनीति में भाग ले सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर अर्थात् जाति, जन्म, वर्ग, वंश, कुल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना वोट डालने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद प्राप्त करने, राजनीतिक दल बनाने तथा सरकार की आलोचना करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
प्रश्न 8.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चार विशेषताएँ बताइए।
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बहुत महत्त्व है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
- भारत एक पूर्ण प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा, जिसका अर्थ है कि भारत अब व्यावहारिक या कानूनी रूप से किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है,
- संविधान में 42वें संशोधन के पश्चात् समाजवाद की स्थापना की गई, जिससे राष्ट्र की उन्नति का लाभ समाज के सब लोगों को प्राप्त हो सके,
- प्रस्तावना में लोकतन्त्र की स्थापना के लिए कहा गया है। संविधान ने प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग को नहीं, अपितु जनता को सौंपी है,
- गणराज्य की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत राज्याध्यक्ष पैतृक न होकर जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होगा।
प्रश्न 9.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त ‘राष्ट्र की एकता’ तथा ‘अखण्डता’ शब्दों का क्या अर्थ है?
उत्तर:
भारतीय संविधान के निर्माता अंग्रेज़ों की ‘फूट डालो’ और शासन करो’ (Divide and Rule) की नीति से भली-भाँति परिचित थे और उसका परिणाम भुगत चुके थे। अतः वे भारत की एकता को बनाए रखने के बहुत इच्छुक थे। अतः संविधान की प्रस्तावना में भारत की एकता की घोषणा की गई। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत के सभी नागरिकों को भारत की (इकहरी) नागरिकता प्रदान की गई है।
भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है तथा सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा ‘एकता’ के साथ ‘अखण्डता’ शब्द को भी जोड़ दिया गया है।
प्रश्न 10.
भारतीय संविधान की त्रुटियाँ या कमियाँ (Weaknesses) बताएँ।
अथवा
किन बातों के आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है?
य संविधान निर्माताओं ने देश की वर्तमान एवं भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए एक अच्छा और स्थायी संविधान बनाने का प्रयास किया, परन्तु फिर भी कोई संविधान ऐसा नहीं हो सकता जो कमियों या दोषों से पूर्णतः मुक्त हो। भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान की भी अनेक आधारों पर आलोचना हुई है। ऐसे कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं-
(1) भारतीय संविधान अत्यधिक लम्बा एवं विस्तृत संविधान है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान न्यायपालिका के सामने वकीलों की वाक्कुशलता से एक खिलौना बनकर रह गया है। अनेक संवैधानिक विवाद खड़े हुए हैं, जिसमें स्वयं न्यायपालिका ने भी अलग-अलग समय में अलग-अलग निर्णय दिए हैं। जैसे मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायपालिका ने अपने निर्णय को बार-बार बदला है,
(2) भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे भी हैं जिनके पीछे कानूनी मान्यता का अभाव । है। ऐसे प्रावधान व्यर्थ में ही संविधान के प्रावधानों को अनावश्यक रूप दे रहे हैं। जैसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त एक अलग अध्याय IV के द्वारा संविधान में रखे गए हैं, परन्तु कानूनी शक्ति के अभाव में न्यायपालिका भी इन्हें लागू करवाने में असमर्थ है। अतः संविधान में केवल कानूनी स्वरूप के प्रावधान रखना ही अधिक अच्छा है,
(3) भारतीय संविधान-निर्मात्री सभा भी वास्तव में सच्चे अर्थों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। आलोचकों का कहना है कि अधिकांश सदस्य विभिन्न सम्पन्न वर्गों से सम्बन्धित थे। अतः वे भारतीय समाज का समुचित प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा नहीं कही जा सकती। ऐसे में उनके द्वारा निर्मित संविधान समस्त जनता का संविधान कैसे कहा जा सकता है।
प्रश्न 11.
भारतीय संविधान की ‘प्रस्तावना’ की आलोचना किन बातों के आधार पर की गई है?
उत्तर:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना दी गई बातों के आधार पर की गई है-
(1) संविधान की प्रस्तावना के आरम्भ में यह बताया जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी नागरिकों द्वारा नहीं चुने गए हैं। उनको चुनने वाला देश की आबादी का एक बहुत छोटा भाग था, क्योंकि सन् 1935 के भारत सरकार के अधिनियम ने सम्पत्ति के आधार पर लोगों को मताधिकार दिया था।
इसलिए आलोचकों का कहना है कि ऐसे सीमित मतदाताओं के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया संविधान जनता का संविधान कैसे कहा जा सकता है, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सभा में 82 प्रतिशत सदस्य काँग्रेस दल के थे तथा काँग्रेस उस समय सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था थी,
(2) संविधान की प्रस्तावना को न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने से न्यायालय उसमें दिए गए सिद्धान्तों को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। अतः उसमें दिए गए सिद्धान्त पवित्र घोषणा से अधिक कुछ भी नहीं हैं,
(3) संविधान के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में दो शब्द जोड़ तो अवश्य दिए हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई सुनिश्चित अर्थ उसमें नहीं दिया है। अतः देश के विभिन्न वर्गों, संगठनों, राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओं द्वारा इन शब्दों का मनमाने अर्थ लगाने से उन्हें व्यावहारिक रूप अभी तक नहीं दिया गया है। समाज में धन की प्रधानता तथा धर्म और जातियों के आधार पर प्रतिदिन होने वाले हिंसक दंगे इस विश्लेषण की पुष्टि करते हैं।
निबंधात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
संविधान के राजनीतिक दर्शन के क्या अर्थ हैं? इसमें प्रायः कौन-कौन सी बातें शामिल होती हैं?
उत्तर:
संविधान के राजनीतिक दर्शन का अर्थ (Meaning of Political Philosophy of the Constitution) वास्तव में संविधान का दर्शन संविधान में अंकित विभिन्न शब्दों एवं धाराओं के वास्तविक अर्थ एवं लक्ष्य को प्रकट करने वाला होता है। दूसरे शब्दों में किसी देश के संविधान का मूल्यांकन जिन आधारों पर किया जाता है, उन्हें ही संविधान के दर्शन का नाम दिया जाता है। संविधान का मूल्यांकन वास्तव में संविधान में निहित उद्देश्यों, आदर्शों एवं मूल्यों की सफलता के आधार पर किया जाता है कि हम इन्हें कहाँ तक प्राप्त करने में सफल हुए और कहाँ तक असफल हुए।
इस प्रकार किसी संविधान का वास्तविक ज्ञान केवल उस देश के संविधान की धाराओं या प्रावधानों के अध्ययन से ही नहीं होता, बल्कि उस दर्शन के अध्ययन से होता है जिस पर उस देश के संविधान की धाराएँ आधारित हैं और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन या सरकार का स्वरूप निश्चित किया गया है।
जैसे हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता एवं समानता प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान की विभिन्न धाराओं में कानूनी प्रावधान किए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा राजनीतिक दर्शन लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर आधारित है। एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में न्याय, समानता एवं स्वतन्त्रता के तत्त्व अपरिहार्य होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान के राजनीतिक दर्शन के आधार पर ही संविधान की सफलताओं एवं कमियों को इंगित किया जा सकता है। संक्षेप में, संविधान का दर्शन संविधान का सार होता है जो एक देश के सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है।
किसी भी देश के संविधान के दर्शन में जो बातें निहित होती हैं वे इस प्रकार हैं-
(1) किसी देश के संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, वे संविधान के दर्शन की ओर संकेत करते हैं, जैसे भारत के संविधान का निर्माण लोकतन्त्र रूपी आदर्श की बुनियाद पर निर्मित हुआ है,
(2) किसी भी देश का संविधान कुछ अवधारणाओं को भी अपने में, अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप निहित रखता है जो उस देश के संविधान के दर्शन की ओर एक संकेत होता है; जैसे भारत में अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, नागरिकता आदि का भारतीय लोकतन्त्र के अनुरूप अर्थ एवं उद्देश्य है। जबकि चीन जैसे साम्यवादी देश में वहाँ के साम्यवादी दर्शन के अनुरूप इन्हीं अवधारणाओं के अर्थ बदल जाते हैं,
(3) एक देश के संविधान का दर्शन वास्तव में उस देश के संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के सम्मुख तत्कालिक परिस्थितियों एवं उसके परिणामस्वरूप उनके बीच हुए वाद-विवाद एवं निर्णयों में भी देखा जा सकता है। जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान में निर्मित होने वाला संविधान एक तरह से ‘शान्ति संविधान’ रूपी दर्शन पर क्यों आधारित हुआ?
इसका उत्तर एवं कारण स्पष्ट है कि द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान की हार एवं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हुई विजित राष्ट्रों की बमबारी से व्यवस्थित तत्कालिक चुनौतियों ने संविधान निर्माताओं को यह निर्णय जापानी जनता के लिए लेना पड़ा कि वे युद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु बल प्रयोग एवं धमकी के साधनों से सर्वथा दूर रहेंगे और न ही सेना व युद्ध सामग्री इत्यादि राष्ट्र के लिए रखेंगे।
जबकि दूसरी तरफ चीनी संविधान का निर्माण भी दूसरे विश्वयुद्ध के बाद हुआ, लेकिन उनकी साम्यवादी विचारधारा के प्रसार की चुनौती ने उन्हें युद्ध एवं राष्ट्रीय सीमाओं के विस्तार को अपने संविधान का निर्माण करते समय अपने राजनीतिक दर्शन में प्रमुख स्थान दिया। इसके अतिरिक्त यहाँ हम एक उदाहरण भारतीय संविधान का भी ले सकते हैं जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद निर्मित हुआ।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने शोषणयुक्त एवं अन्याय एवं अत्याचार पर आधारित जीवन ब्रिटिश शासकों के अधीन व्यतीत किया था। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं की चुनौतियाँ विशेषकर भारतीय नागरिक को गौरवमय जीवन के साथ-साथ न्याय, समानता एवं स्वतन्त्रता पर आधारित जीवन प्रदान करना था। अतः भारतीय संविधान एवं उसकी शासन-प्रणाली वास्तव में ऐसे ही राजनीतिक दर्शन पर आधारित है,
(4) किसी देश के संविधान का दर्शन वास्तव में देश की सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति एवं उसके सम्प्रभु सम्पन्न स्वरूप के साथ-साथ उस देश के नागरिकों के साथ उनके सम्बन्धों को भी स्पष्ट करता है। जैसे भारत का संविधान न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के साथ व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जबकि चीन में न्यायपालिका एक अधीनस्थ संस्था या अंग के रूप में कार्य करती हुई विधानपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की ही पुष्टि करने का कार्य करती है। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि किसी देश के संविधान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसके वैधानिक स्वरूप के साथ-साथ संविधान में निहित आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप उसका मूल्यांकन किया जाए। यहाँ हम संविधान के दर्शन की स्पष्टता हेतु विशेषतः भारतीय संविधान में निहित मूल्यों एवं आदर्शों की स्पष्टता हेतु संविधान के मूल प्रावधानों का भी अध्ययन करेंगे।
प्रश्न 2.
भारतीय संविधान के मूल प्रावधानों (Core Provisions) का उल्लेख करें।
उत्तर:
किसी भी देश का संविधान न केवल शासक एवं शासित सम्बन्धों को निश्चित करता है, बल्कि एक वैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अधीन नागरिकों एवं समाज के विकास सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए शासन शक्ति या सरकार के प्रभुसत्ता सम्पन्न अंगों के कार्यों एवं उनकी शक्तियों की भी स्पष्ट व्याख्या करता है। यही वास्तव में उस देश के संविधान के सारभूत या मूल प्रावधान होते हैं। यहाँ हम भारतीय संविधान के मूल प्रावधानों का विवेचन करेंगे जो निम्नलिखित हैं
1. सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक, गणराज्य की स्थापना (Establishment of a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic)-भारत में संविधान के द्वारा भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इसमें समाजवादी (Socialist) तथा धर्म-निरपेक्ष (Secular) शब्दों को जोड़कर इसे सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य बना दिया गया है। इन विभिन्न अवधारणाओं को संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा रहा है
(1) सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न (Sovereign):
सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न का अर्थ यह है कि भारत अपने आन्तरिक तथा बाहरी दोनों ही प्रकार के मामलों में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च सत्ताधारी है। आन्तरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि भारत क्षेत्र में रहने वाले लोगों और भारत राज्य में स्थित सभी समुदायों पर भारत राज्य को अधिकार प्राप्त है और बाहरी प्रभुसत्ता का अभिप्राय यह है कि भारत किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है
तथा दूसरे राज्यों से वह अपनी इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। 15 अगस्त, 1947 से पूर्व भारत को यह स्थिति प्राप्त नहीं थी। लेकिन 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है और यह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
(2) समाजवादी (Socialist):
समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इस शब्द का उद्देश्य है कि भारत में इस प्रकार की शासन-व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे समाज के सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को, विकास के लिए उचित तथा समान अवसर प्राप्त हों, मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त हो और आर्थिक विषमता को कम किया जाए।
कांग्रेस ने बहुत पहले से ही भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था और उसी दल की सरकार द्वारा यह शब्द संविधान में 1976 (42वें संशोधन द्वारा) में जोड़ दिया गया।
(3) धर्म-निरपेक्ष (Secular):
धर्म-निरपेक्ष शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और धर्म के आधार पर राज्य किसी प्रकार के भेदभाव का प्रयोग नहीं करेगा।
सरकार किसी भी धर्म को कोई विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को कोई ऐसा चंदा या कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए खर्च की जाने वाली हो। यद्यपि हमारे संविधान में धर्म-निरपेक्षता की ओर पहले से ही संकेत था, परन्तु अब यह शब्द जोड़ने से संविधान का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया है।
(4) लोकतन्त्रात्मक (Democratic):
लोकतन्त्रात्मक का अर्थ है कि भारत एक लोकतन्त्रात्मक राज्य है, जिसमें अन्तिम शक्ति जनता के हाथों में है। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उस काल के लिए देश के शासन को चलाते हैं। अब तक देश में हुए 17 लोकसभा चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि यदि सरकार अपने उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य ठीक तरह से नहीं करती है तो उस सरकार या मन्त्रिमण्डल को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात् संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं और उनकी रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।
(5) गणराज्य (Republic):
गणराज्य का अर्थ यह है कि देश का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होगा। हमारे देश के मुखिया अर्थात् राष्ट्रपति का पद पैतृक सिद्धान्त पर आधारित नहीं है, वह एक निश्चित काल (5 वर्ष) के लिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो 6 मास के अन्दर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है।
संघात्मक संविधान परन्तु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव (Federal Constitution with a Unitary Bias) यद्यपि भारतीय संविधान में ‘संघ’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परन्तु फिर भी यह सत्य है कि भारत का वर्तमान संविधान देश में संघीय शासन-प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें वे सभी लक्षण मौजूद हैं जो संघीय सरकार की स्थापना के लिए आवश्यक हैं; जैसे
(1) संविधान के अनुसार शासन की शक्तियों का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के द्वारा बँटवारा किया गया है।
(2) भारत का संविधान लिखित है तथा इसका अधिकांश भाग कठोर है। इसका कारण यह है कि संविधान का एक बहुत बड़ा. भाग ऐसा है, जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है।
(3) संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसकी रक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के उल्लंघन में पास किए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित करके रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
(4) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संसद का संगठन द्वि-सदनीय विधानमण्डल प्रणाली के आधार पर किया गया है। लोकसभा, जो कि संसद का निचला सदन है, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा में संघ की इकाइयों के प्रतिनिधि बैठते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संविधान में संघीय शासन-प्रणाली के सभी तत्त्व मौजूद हैं,
अतः यह संघीय संविधान है। कुछ आलोचकों का विचार है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, क्योंकि इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार को इतना अधिक शक्तिशाली बनाया गया है कि यह संविधान बनावट में संघात्मक है, परन्तु भाव में एकात्मक है। पी०एस० देशमुख का मत था कि, “जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है।” भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण संक्षेप में निम्नलिखित हैं-
(1) भारतीय संविधान ने एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र का निर्माण किया है। डॉ० कश्यप के अनुसार, “संघ सूची में 97 विषय हैं और वह तीनों सूचियों में सबसे लम्बी है। समवर्ती सूची में 52 विषयों पर भी केन्द्र सरकार जब चाहे कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्रीय सरकार में ही निहित हैं।”
(2) संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना भी एकात्मक शासन-प्रणाली का लक्षण है।
(3) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के संघात्मक स्वरूप का एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाना एकात्मक शासन का लक्षण है।
(4) देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था का होना भी एकात्मक शासन का लक्षण है।
(5) समूचे देश के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवाएँ एवं एक ही चुनाव आयोग की व्यवस्था भी देश को एकात्मक शासन की ओर ले जाता है।
(6) देश के नागरिकों को केवल इकहरी नागरिकता प्रदान करना भी एकात्मक शासन का ही लक्षण है।
अतः संविधान में एकात्मक लक्षणों को देखने के पश्चात् यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक होने के पश्चात् भी यह कहा जा सकता है कि यह एकात्मक स्वरूप की ओर झुका हुआ है।
अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर (Partly Flexible and Partly Rigid)-भारत का संविधान इतना कठोर नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और न ही इतना लचीला है जितना कि इंग्लैण्ड का संविधान। यह अंशतः लचीला (Flexible) और अंशतः कठोर (Rigid) है। वास्तव में हमारे संविधान-निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि संविधान इतना लचीला न हो कि यह बहु-संख्यक दल के हाथों में खिलौना बन जाए। दूसरी ओर यह इतना कठोर भी न हो कि इसे देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदला न जा सके, जिससे इसकी प्रगति के मार्ग में बाधा आए।
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए तीन विभिन्न प्रणालियों को अपनाया गया है। सर्वप्रथम, संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में संशोधन संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इस श्रेणी में नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा उनका पुनर्गठन, राज्य विधानमण्डलों का संगठन एक-सदनीय अथवा द्वि-सदनीय आधार पर करना तथा भारतीय नागरिकता से सम्बन्धित विषय शामिल हैं। दूसरे स्थान पर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकार होने के पश्चात् इसका कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।
इस श्रेणी में राष्ट्रपति के चुनाव की ‘पद्धति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से सम्बन्धित विषय तथा राज्यों के संसद में प्रतिनिधित्व आदि विषय आते हैं। संविधान में दिए गए शेष विषयों के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है और न ही पूर्ण रूप से कठोर, बल्कि इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाता है। अब तक भारतीय संविधान में 104 (दिसम्बर, 2019 तक) संशोधन हो चुके हैं।
4. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)-भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अनुसार, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। ये वे अधिकार हैं जो एक मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक समझे जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इन अधिकारों की न केवल संविधान में घोषणा ही की गई है, वरन उन्हें लागू करने के लिए भी उचित साधन जुटाए गए हैं। ये अधिकार न्याययोग्य (Justiciable) हैं और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को उनकी रक्षा का कार्य सौंपा गया है।
उन्हें विधानमण्डल द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को अथवा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी ऐसे अध्यादेश को अवैध घोषित करने तथा रद्द करने का अधिकार दिया गया है, जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हों। प्रत्येक नागरिक अपने इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालयों की सहायता ले सकता है और उसका यह अधिकार, केवल संकटकालीन स्थिति को छोड़कर, कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। .. संविधान के भाग तीन, अनुच्छेद 14 से 32 तक नागरिकों के निम्नलिखित छः अधिकारों का वर्णन किया गया है
- समानता का अधिकार (Right to Equality)
- स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
- धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
- सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)
- सवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ये अधिकार असीमित नहीं हैं। इनके प्रयोग पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त संसद इनमें संशोधन करके इन पर रोक लगा सकती है।
5. मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)-संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51-A में नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का समावेश पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होते हुए किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के पश्चात् भारतीय संविधान में निम्नलिखित दस मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया
- संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- स्वतन्त्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना तथा उनका पालन करना।
- भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखण्डता का समर्थन एवं रक्षा करना।
- देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना।
- धार्मिक, भाषायी तथा प्रादेशिक विभिन्नताओं को त्यागकर भारत के सभी लोगों में मेल-मिलाप तथा बन्धुत्व की भावना विकसित करना, स्त्रियों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
- अपनी मिली-जुली संस्कृति की सम्पन्न परम्परा का सम्मान करना तथा उसे सुरक्षित रखना।
- वनों, झीलों, नदियों तथा अन्य जीवों सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीव-जन्तुओं के प्रति दया की भावना रखना।।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना।
- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना।
- व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य-कलापों के क्षेत्र में कुशलता लाने का प्रयत्न करना, ताकि राष्ट्र उपलब्धि के उच्च
शिखरों तक पहुँच सके। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सन् 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या संरक्षकों को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी कर्त्तव्य को निश्चित किया गया है। इस प्रकार अब मूल कर्त्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।
6. राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy):
भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन संविधान के भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन सिद्धान्तों को अपनाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैण्ड के संविधान की नकल की है।
ये सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में हैं और इनके द्वारा उन्हें यह आदेश दिया गया है कि वे अपनी नीति का निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखें, क्योंकि इन सिद्धान्तों के पूर्ण रूप से अपनाए जाने पर ही भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है।
इन सिद्धान्तों का उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त न्यायसंगत (Justiciable) नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि ये सिद्धान्त न्यायालयों द्वारा कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते और यदि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारें उन्हें लागू नहीं करती अथवा उन्हें ध्यान में रखकर कार्य नहीं करतीं, तो नागरिकों को न्यायालय में जाकर उनके विरुद्ध न्याय माँगने का अधिकार नहीं है।
7. संयुक्त चुनाव-प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार (Joint Electorate and Universal Adult Franchise):
भारत के नए संविधान के अनुसार पृथक् तथा साम्प्रदायिक प्रणाली (Separate and Communal Electorate), जिसका आरम्भ भारत में सन् 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और जिसका विस्तार सन् 1919 तथा 1935 के अधिनियमों के द्वारा किया गया था, को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर संयुक्त चुनाव-प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा देश में साम्प्रदायिकता को कम करने के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में मताधिकार बहुत ही सीमित था, जो सम्पत्ति, शिक्षा तथा कर देने आदि की योग्यताओं पर आधारित था, परन्तु नए संविधान के अनुसार, इस प्रकार के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है।
अब मताधिकार के लिए व्यक्ति की आयु ही एकमात्र योग्यता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के यह अधिकार दिया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी जोकि 61वें संवैधानिक संशोधन (1989) के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
8. इकहरी नागरिकता (Single Citizenship):
भारत में संघीय शासन-व्यवस्था की स्थापना के बावजूद प्रत्येक नागरिक को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह देश के किसी भी भाग में (किसी भी राज्य में) रहता हो, भारत का ही नागरिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कुछ अन्य संघ-राज्यों में दोहरी नागरिकता के सिद्धान्त को अपनाया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने के साथ-साथ उस राज्य-विशेष का भी नागरिक है, जिसमें वह निवास करता है, परन्तु भारतीय संविधान के निर्माताओं का यह भी विचार था कि दोहरी नागरिकता देश की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः उन्होंने संघीय व्यवस्था की स्थापना करते हुए भी इकहरी नागरिकता के सिद्धान्त को अपनाया है।
9. स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary):
भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि इसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुरक्षित किया गया है। संघात्मक शासन-व्यवस्था में संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतन्त्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु भी । न्यायपालिका की स्वतन्त्रता आवश्यक हो जाती है। इस कारण से हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए अनेक व्यवस्थाएँ की गई हैं।
10. द्वि-सदनीय विधानमण्डल (Bicameral Legislature):
संसार के अन्य संघीय संविधानों की भान्ति भारतीय संविधान के द्वारा भी संघीय स्तर पर द्वि-सदनीय विधानमण्डल की स्थापना की गई है। संसद के दो सदन हैं लोकसभा (House of the People) तथा राज्यसभा (Council of States)। लोकसभा संसद का निचला सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 तथा कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। राज्यसभा में अधिक-से-अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से.12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत (Nominate) किए जाते हैं और शेष सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् इसके 1/3 सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा में देश की जनता तथा राज्यसभा में भारतीय संघ की इकाइयों (राज्यों) को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
11. अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था (Special Provisions for the Welfare of Minorities and Backward Classes):
संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके लिए सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में स्थान आरक्षित रखे गए हैं।
79वें सवैधानिक संशोधन द्वारा यह अवधि 2010 तक तथा 95वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान सन् 2020 तक बढ़ा दिया गया था जो 104वें संवैधानिक द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान जनवरी, 2030 तक बढ़ा दिया गया। पिछड़े वर्गों को यह सुविधा इसलिए दी गई है कि इनकी बहुत पिछड़ी स्थिति के कारण इन्हें विकास के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है।
12. एक राष्ट्र भाषा (One National Language):
भारत एक विशाल देश है, जिसमें अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इसलिए संविधान के द्वारा 22 भाषाओं (92वें संशोधन के पश्चात) को मान्यता दी गई है, परन्तु देश की एकता को बनाए रखने के लिए तथा विभिन्न भाषायी प्रान्तों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के महत्त्व को आवश्यक समझा गया, इसलिए हिन्दी को देवनागरी लिपि में राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है। हिन्दी के विकास के लिए केन्द्र तथा राज्यों को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।
13. कानून का शासन (Rule of Law):
भारत के संविधान की यह भी विशेषता है कि इसके द्वारा कानून के शासन की व्यवस्था की गई है। कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अमीर-गरीब, पढ़े-लिखे तथा अनपढ़, कमजोर और शक्तिशाली सभी देश के कानून के समक्ष बराबर हैं। कानून से ऊँचा कोई नहीं है। जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानून के द्वारा ही सजा दी जाती है। कानूनी कार्रवाई किए बिना किसी व्यक्ति को बन्दी नहीं बनाया जा सकता।
14. पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की संवैधानिक व्यवस्था (Constitutional Provision of Panchayats and Municipalities):
संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों की तथा 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। ये दोनों संशोधन सन 1992 में पारित किए गए। इन संशोधनों द्वारा पहली बार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है।
15. विश्व-शान्ति का समर्थक (It Supports World Peace):
भारतीय संविधान विश्व-शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक है। राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों में यह कहा गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रबल समर्थक है तथा राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की उन्नति और राष्ट्रों के बीच न्याय एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा।
व्यवहार में भी भारत द्वारा विश्व-शान्ति बनाए रखने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है और युद्ध केवल उसी समय किए गए, जब आत्मरक्षा हेतु ऐसा करना आवश्यक हो गया था।
16. संकटकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers) भारतीय संविधान में हमारे संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति को विशेष रूप से आपात्कालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं
(1) संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण या इनमें से किसी भी एक के होने की सम्भावना हो तो राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भाग विशेष में संकटकालीन घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा होने पर उसका नाममात्र का स्वरूप वास्तविक शासक के स्वरूप में बदल जाता है।
(2) किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल होने या ऐसी सम्भावना होने पर भी उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्य की शासन-व्यवस्था को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति सीधे अपने हाथों में ले लेता है।
(3) संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत यदि देश में वित्तीय संकट का भय हो तो राष्ट्रपति आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है। अतः दिए गए सारभूत प्रावधान भारतीय संविधान के वैधानिक स्वरूप को स्पष्ट करने के साथ भारतीय समाज में नागरिकों हेतु शासन-व्यवस्था के स्वरूप एवं उद्देश्यों को भी स्पष्ट करते हैं। परन्तु यहाँ हम संविधान के मूल प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान में की गई उन परिकल्पनाओं को जो संविधान-निर्माता भावी भारत के निर्माण के सन्दर्भ में रखते थे, का विवेचन करना भी बहुत उपयुक्त होगा। यहाँ हम उन्हीं परिकल्पनाओं का विवेचन कर रहे हैं।

प्रश्न 3.
प्रस्तावना (Preamble) से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करें।
उत्तर:
प्रस्तावना का अर्थ (Meaning of Preamble)-किसी भाषण अथवा लेख में प्रारम्भिक अथवा परिचयात्मक कथन को प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना किसी संविधान अथवा अधिनियम का वह प्रारम्भिक कथन है जिसमें उसके निर्माण के कारणों का उल्लेख किया जाता है तथा उन उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है।
उसमें संविधान के स्रोत को इंगित किया जाता है तथा उस तिथि का उल्लेख किया जाता है जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। प्रस्तावना का स्थान प्रस्तावना का स्थान किसी संविधान अथवा अधिनियम के शीर्षक के बाद और उसके मुख्य भाग से पहले होता है। अतः संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा झरोखा होती है, जिसमें संविधान के निर्माताओं की भावनाओं तथा उनकी आशाओं का दृश्य देखा जा सकता है। इसी कारण से भारतीय संविधान की प्रास्तावना को संविधान-निर्माताओं के दिलों की कुंजी’ कहा जाता है।
प्रस्तावना में संशोधन-प्रायः यह विचार प्रकट किया जाता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं था, परन्तु सन् 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के केशवानन्द भारती बनाम भारत सरकार, नामक मुकद्दमे का फैसला देते हुए इसका स्पष्टीकरण कर दिया। जिसके अनुसार, प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद को, इसके मूल ढाँचे (Basic Structure) को छोड़कर अन्य भागों में संशोधन करने का अधिकार है।
इसके परिणामस्वरूप सन् 1976 में भारतीय संसद ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके इसमें समाजवादी (Socialist) तथा धर्म-निरपेक्ष (Secular) शब्द जोड़ दिए थे। इसके अतिरिक्त जहाँ ‘राष्ट्र की एकता’ के शब्द का प्रयोग किया गया, वहाँ ‘एकता तथा अखण्डता’ (Unity and Integrity) का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में यह शब्द जोड़कर यह सिद्ध किया गया है कि हम देश में समाजवाद लाने और राज्य को धर्म-निरपेक्ष बनाए रखने के लिए पूरी तरह उत्सुक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है
“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म-समर्पित करते हैं।” प्रस्तावना की विशेषताएँ या प्रस्तावना की व्याख्या-भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं या इसकी व्याख्या करने के लिए हम उपर्युक्त प्रस्तावना को निम्नलिखित तीन शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित कर सकते हैं
- संवैधानिक शक्ति के स्त्रोत (Source of Constitutional Authority),
- भारतीय शासन का स्वरूप (Nature of Indian Government)
- संविधान के उद्देश्य (Aims of the Constitution)। उपर्युक्त तीनों शीर्षकों का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित है
1. संवैधानिक शक्ति के स्रोत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रारम्भिक एवं अन्तिम शब्द, “हम भारत के लोग ……… संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं”, शब्दों से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। प्रथम, संविधान के द्वारा अन्तिम प्रभुसत्ता भारत की जनता में निहित की गई है; द्वितीय, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं तथा तृतीय, संविधान निर्माता भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और जनता द्वारा ही
इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस सम्बन्ध में डॉ०बी०आर० अम्बेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) ने संविधान सभा की बहस में ठीक ही कहा था, “मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार यह प्रकट करती है कि इस संविधान का आधार, इसकी शक्ति तथा प्रभुसत्ता इसे लोगों से ही प्राप्त हुई है।”
2. भारतीय शासन का स्वरूप संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रीय गणराज्य घोषित किया गया है, जो भारतीय शासन-व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त भारतीय शासन-व्यवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले शब्दों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है
(1) सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न का अर्थ है कि भारत पर आन्तरिक अथवा बाहरी दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा रूस आदि देशों की भाँति भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि अथवा समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्रमण्डल का सदस्य होना इसकी प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता।
(2) समाजवादी शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि भारत में शासन-व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए कि सभी वर्गों को विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्गों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण तथा परिस्थितियाँ मिलें, आर्थिक असमानता कम और देश के विकास का फल थोड़े से लोगों के हाथों में न होकर समाज के सभी लोगों को मिले।
(3) धर्म-निरपेक्ष शब्द भी प्रस्तावना में सन् 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार, किसी भी धर्म को अपनाने तथा उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता और राज्य किसी विशेष धर्म की किसी विशेष रूप से सहायता नहीं कर सकता। धर्म के आधार पर किसी सरकारी शिक्षा-संस्था में किसी को दाखिला देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
(4) लोकतन्त्रीय शब्द का अर्थ है कि शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में है। शासन चलाने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी धर्म, जाति अथवा स्थान से सम्बन्ध रखता हो, राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्रदान किए गए हैं। साम्प्रदायिक चुनाव-प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
(5) गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत में राज्य के अध्यक्ष का पद वंश-क्रमानुगत (Hereditary) नहीं है, बल्कि राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्रपति एक निश्चित काल के लिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इंग्लैण्ड तथा जापान लोकतन्त्रीय राज्य होते हुए भी, गणराज्य नहीं हैं क्योंकि इन देशों में राजा का पद पैतृक आधार पर चलता है और वह जनता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित काल के लिए निर्वाचित नहीं किया जाता।
3. संविधान के उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह बात भी स्पष्ट होती है कि संविधान द्वारा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की आशा की गई है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं
(1) न्याय-संविधान का उद्देश्य यह है कि देश के सभी नागरिकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र- सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय मिले। इस बहुमुखी न्याय से ही नागरिक अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है। .
(क) सामाजिक न्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्म-स्थान, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित किया गया है। देश के सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए नागरिकों में रंग, जाति व धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी पाने के क्षेत्र में सभी के लिए समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है।
(ख) आर्थिक न्याय का यह अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपनी आजीविका कमाने के समान तथा उचित अवसर प्राप्त हों तथा उन्हें अपने कार्य के लिए उचित वेतन मिले। आर्थिक न्याय के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन तथा वितरण के साधन थोड़े-से व्यक्तियों के हाथों में न होकर समाज के हाथों में हों और उनका प्रयोग समस्त समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया जाए। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना के आधार पर ही की जा सकती है।
(ग) राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाकर इस व्यवस्था को लागू किया गया है। धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है और साम्प्रदायिक चुनाव-प्रणाली का अन्त कर दिया गया है।
(2) स्वतन्त्रता भारतीय संविधान का उद्देश्य नागरिकों को केवल न्याय दिलाना ही नहीं बल्कि स्वतन्त्रता को भी निश्चित करना है, जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा उपासना (Thought, Expression, Faith and Worship) की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है। इसकी पूर्ति संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के द्वारा की गई है।
(3) समानता प्रस्तावना में सामाजिक स्तर तथा अवसर (Social Status and Opportunity) का उल्लेख किया गया है। स्तर . की समानता का अर्थ यह है कि कानून की दृष्टि में देश के सभी नागरिक समान हैं तथा किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नही हैं
संविधान का राजनीतिक दर्शन और धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन बातों का स्पष्टीकरण संविधान की धाराओं – 14-18 के द्वारा किया गया है। धारा 14 के अन्तर्गत सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता तथा सुरक्षा प्रदान की गई है। धारा 15 में यह कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, रंग, जाति तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
धारा 16 के द्वारा सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। धारा 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है तथा धारा 18 के द्वारा शिक्षा तथा सेना की उपाधियों को छोड़ अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अन्त कर दिया गया है।
(4) बन्धुता-संविधान की प्रस्तावना में बन्धुता की भावना को विकसित करने पर भी बल दिया गया है। भारत जैसे देश के लिए, जिसमें गुलामी के लम्बे काल के कारण धर्म, जाति व भाषा आदि के आधार पर भेदभाव उत्पन्न हो गए थे, बन्धुता की भावना के विकास का विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से ही साम्प्रदायिक चुनाव-प्रणाली तथा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है।
इसके साथ ही प्रस्तावना में ‘व्यक्ति की गरिमा’ (Dignity of Individual) शब्दों का रखा जाना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत पवित्र है। इसी धारणा से देश के सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
(5) राष्ट्र की एकता व अखण्डता भारतीय संविधान के निर्माता अंग्रेज़ों की ‘फूट डालो व शासन करो’ (Divide and Rule) की नीति से अच्छी प्रकार परिचित थे, इसलिए उनके मन और मस्तिष्क में राष्ट्र की एकता का विचार बहुत प्रबल था। इसी कारण से संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की घोषणा की गई।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है तथा इकहरी नागरिकता (Single Citizenship) के सिद्धान्त को अपनाया गया है। समस्त देश का एक ही संविधान है तथा संविधान में अनेक (22) भाषाओं को मान्यता दी गई है। 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्र की एकता के साथ अखण्डता शब्द जोड़ दिया गया है।
प्रश्न 4.
भारत के भावी संविधान (शासक-व्यवस्था) के बारे में संविधान सभा की परिकल्पनाएँ क्या थीं?
उत्तर:
भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों की स्वतन्त्र भारत के भावी राज्य-प्रबन्ध के बारे में क्या परिकल्पनाएँ थीं। इनकी पृष्ठभूमि को सन् 1928 में प्रकाशित हुई नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report, 1928) में देखा जा सकता है। डॉ० सरकारिया ने नेहरू रिपोर्ट को ‘वर्तमान संविधान की रूप-रेखा’ (Blue print of the Present (Indian) Constitution) कहा है।
यह रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया पहला प्रयत्न था। उसके पश्चात् संविधान सभा में पं० जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ (Objective Resolution) रखा। वह भी संविधान सभा के सदस्यों के विचारों का दर्पण था।
इसी तरह संविधान की प्रस्तावना में भी संविधान सभा के भावी भारत के राज्य-प्रबन्ध से सम्बन्धित धारणाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। अतः उद्देश्य, प्रस्ताव और संविधान की प्रस्तावना उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर इंगित करते हैं जिनके आधार पर संविधान सभा के सदस्य भावी भारत की शासन-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। संविधान सभा के सदस्यों की भारत की भावी शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का वर्णन निम्नलिखित है-
1. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की परिकल्पना-भारतीय नेता मुख्य रूप से उस वर्ग से सम्बन्ध रखते थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी देखी थी, इसलिए उनकी इच्छा भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य देखने की थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व सम्पन्न राज्य घोषित किया। इसका अभिप्राय यह है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। वह किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। प्रभुसत्ता जनता के पास है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करे।
2. प्रजातन्त्र की परिकल्पना भारतीय संविधान सभा की दूसरी परिकल्पना यह थी कि भारत में प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना की जाए। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य प्रजातन्त्र के समर्थक थे। अतः उन्होंने भारत के लिए प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था को अपनाया। इसका अर्थ यह है कि शासन की अन्तिम शक्ति जनता के हाथ में ही रहेगी।
लोग शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक 18 वर्ष के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया है और निर्वाचित होने का अधिकार भी दिया गया है। कानून के शासन की व्यवस्था तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।
3. समाजवाद की परिकल्पना-भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पर समाजवाद की अवधारणा का प्रभाव था, इसलिए वे भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। नेहरू जी भारत में समाजवाद स्थापित करने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि भारत के विकास का मार्ग केवल समाजवाद में ही निहित है। यद्यपि संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को नहीं रखा गया था, लेकिन सन् 1976 में संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ दिया गया है। वास्तविकता में कांग्रेस पहले से ही भारत में प्रजातन्त्रीय समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य घोषित कर चुकी थी। समाजवाद का अर्थ है कि भारत में इस प्रकार से
सन-व्यवस्था चलाई जाए जिसमें आर्थिक असमानता न हो तथा इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया जाए जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपना विकास करने के अवसर प्राप्त हों। देश के विकास का फल कुछ थोड़े-से लोगों के हाथ में न रहकर समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के प्राप्त हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, संविधान में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों को अंकित किया गया है। यही नहीं समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 42वां संशोधन पास किया गया जिसके अन्तर्गत निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान की गई है।
4. गणराज्य बनाने की परिकल्पना भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष, किस प्रकार की शासन-व्यवस्था अपनाई जाए, इस सम्बन्ध में कई विकल्प थे। कुछ सदस्य अमेरिका की भाँति अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था अपनाने के पक्ष में थे। लगभग 8 सदस्यों ने शक्ति पृथक्करण के आधार पर अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली अपनाए जाने का समर्थन किया।
इसके विपरीत कुछ सदस्य संसदीय शासन-व्यवस्था को अंगीकार करने के पक्ष में थे। अन्त में संसदीय सरकार अपनाए जाने का निर्णय किया गया, परन्तु संसदीय सरकार जरूरी नहीं है कि वह गणराज्य भी हो; जैसे इंग्लैण्ड और जापान में संसदीय सरकार तो है, परन्तु गणराज्य नहीं है। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने भारत में गणराज्य स्थापित करने का निर्णय लिया।
गणराज्य की प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसमें राज्य का मुखिया नाममात्र का अधिकारी होता है, जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन-मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है।
5. धर्म-निरपेक्ष राज्य व्यवस्था की परिकल्पना-संविधान सभा के सदस्य इस बात से भली-भाँति परिचित थे कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म, वर्ग व जाति के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों में मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का एकमात्र साधन धर्म-निरपेक्षता है। इसलिए उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि भारत की भावी शासन-व्यवस्था धर्म-निरपेक्षता की नींव पर आधारित हो।
अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यही नहीं धर्म-निरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक प्रचार पर रोक लगाई गई है।
6. कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना-राष्ट्रीय आन्दोलन राजनीति आन्दोलन होने के साथ-साथ सामाजिक व आर्थिक आन्दोलन भी था। राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत नेताओं द्वारा भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। इन सभी प्रयत्नों का संविधान सभा के सदस्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कामना की कि भारत एक ऐसा कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिले।
कल्याणकारी राज्य की धारणा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 38 में किया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को उद्देश्य, प्रस्ताव और संविधान की प्रस्तावना में भी देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, वंश, लिंग व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत के कलंक को समाप्त किया गया है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए समान अवसर प्राप्त हों एवं उसके कार्य के लिए उसे उचित वेतन मिले तथा उसका आर्थिक शोषण न हो।
इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान के अनुच्छेद 38 एवं 39 में राज्य-न की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 के अनुसार बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा अंगहीन होने की अवस्था में राज्य की ओर से सहायता की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
7. शक्तिशाली केन्द्र की परिकल्पना-राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतागण तत्कालीन साम्प्रदायिक तत्त्वों तथा उनकी गतिविधियों से भली-भाँति अवगत थे और इसी साम्प्रदायिकता के कारण भारत का दो भागों में विभाजन हुआ। संविधान निर्माता ने ऐसा सोचा था कि विभाजन के बाद साम्प्रदायिकता का दानव समाप्त हो जाएगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। विभाजन शक्तियों ने अपना सिर फिर से उठाना आरम्भ कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि इसका एकमात्र उपचार शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था है।
इस प्रकार के वाद-विवाद के उपरान्त भारत में शक्तिशाली केन्द्र के अधीन संघात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्त्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर भारतीय शासन-व्यवस्था संघात्मक है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे तत्त्व भी पाए जाते हैं जिनके आधार पर भारतीय शासन-व्यवस्था एकात्मक है। इसी सन्दर्भ में के०सी० वीयर (K.C. Weare) ने कहा है, “भारत एक एकात्मक राज्य है, जिसमें संघात्मक लक्षण हैं।” इसी प्रकार जैनिंग्स (Jennings) ने विचार व्यक्त किए हैं, “भारत शक्तिशाली केन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियों वाला संघात्मक राज्य है।” पण्डित नेहरू ने भी संविधान सभा में बोलते हुए शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना का समर्थन किया था।
8. स्वतन्त्रता, समानता व बन्धुत्व की परिकल्पना मनुष्य की उन्नति व विकास के लिए केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता ही काफी नहीं है, बल्कि अन्य स्वतन्त्रताएँ, समानता व बन्धुत्व भी आवश्यक हैं। संविधान सभा के सदस्य स्वतन्त्रता, समानता व बन्धुत्व की भावना के महत्त्व से भली-भाँति अवगत. थे। अतः वे इनको भारत के संविधान में समावेश करने के पक्ष में थे। उद्देश्य, प्रस्ताव व संविधान की प्रस्तावना में स्वतन्त्रता, समानता व बन्धुत्व के महत्त्व पर बल दिया गया है। संविधान में नागरिकों को कई प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं; जैसे विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता आदि। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में विभिन्न समानताओं का समावेश किया गया है;
जैसे कानून के समक्ष समानता, जाति, रंग, लिंग व भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न करना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समानता, शिक्षा व सैनिक उपाधियों को छोड़कर शेष उपाधियों की समाप्ति आदि । संविधान के निर्माता फ्रांस की क्रान्ति के नारे, स्वतन्त्रता, समानता के साथ-साथ बन्धुत्व के नारे से भी प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बन्धुत्व की भावना को विकसित करने पर बल दिया।
डॉ०.अम्बेडकर (Dr. Ambedkar) के अनुसार, “बन्धुता एक ऐसा सिद्धान्त है जो सामाजिक जीवन को एकता और मजबूती प्रदान करता है।” इसी सन्दर्भ में एम०वी० पायली (M.V. Pylee) का कथन है, “न्याय, स्वतन्त्रता और समानता के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण करने का उद्देश्य था कि सब यह समझें कि वे एक ही धरती तथा एक ही जन्मभूमि की सन्तान हैं और आपस में बन्धु हैं।”
9. राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की परिकल्पना संविधान को बनाने वाले अंग्रेज़ों की इस ‘फूट डालो और शासन करो’ (Divide and Rule) की नीति से भली-भाँति परिचित थे। अंग्रेजों की इसी नीति के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसलिए संविधान निर्माता भारत की एकता को बनाए रखने के पक्ष में थे। वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की घोषणा की गई तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाया गया। सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई।
समस्त भारत के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया तथा 18 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, किन्तु अब भारतीय में संविधान में चार भाषाओं (मैथिली, डोगरी, बोडो और सन्थाली) को और जोड़ दिया गया है। अब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल गई है। नवम्बर, 1976 में हुए 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के साथ अखण्डता (Integrity) शब्द जोड़ा गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है तथापि इन्हें राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए निलम्बित भी किया जा सकता है।
10. व्यक्तिगत गौरव विषयक परिकल्पना संविधान सभा के सदस्य अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से भली-भाँति परिचित थे। स्वाधीनता से पहले अंग्रेजों ने भारतीयों के गौरव को मान्यता प्रदान नहीं की थी। विदेशों में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। स्वाधीनता के बाद भारतीयों में गौरव को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में इस बात को अंकित किया गया है कि बिना गौरव अनुभव किए कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता।
इस तरह से संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत में व्यक्तिगत गौरव को स्थापित किया जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा सब व्यक्तियों को मौलिक अधिकार समान रूप से प्रदान करना, भारतीयों के व्यक्तिगत गौरव को ऊँचा उठाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। मौलिक अधिकारों के अलावा मताधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार भारतीयों में व्यक्तिगत गौरव एवं स्वाभिमान को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है।
11. अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा सम्बन्धी परिकल्पना स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में पिछड़ी जातियों व वर्गों .. की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1/5 भाग थी जिन्हें अपमान व तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता था। श्री अम्बेडकर स्वयं इसी वर्ग से सम्बन्धित थे और उन्हें अपमान व तिरस्कार का कटु अनुभव था।
इसलिए वे पिछड़े वर्गों व जातियों के लिए कुछ करने के लिए कटिबद्ध थे। यही नहीं संविधान सभा के अन्य सदस्य भी पिछड़ी जातियों व वर्गों के उत्थान के लिए किए जाने वाली व्यवस्था के पक्ष में थे। भारतीय संविधान में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा के विशेष अनुच्छेद लिखे गए हैं। इन श्रेणियों के लोगों के लिए संविधान में यह लिखा गया है कि केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें उनके लिए कुछ सरकारी नौकरियाँ आरक्षित रखेंगी।
इसी तरह उनके लिए संसद तथा प्रान्तीय विधानपालिकाओं की कुछ सीटें भी आरक्षित की गई हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में दो ऐंग्लो-इण्डियन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। शुरू में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित व पिछड़ी जातियों तथा कबीलों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था सन् 1960 तक की गई थी। बाद में दस-दस वर्ष करके इस अवधि को कई बार बढ़ा दिया गया।
अब 104वें संशोधन द्वारा इस अवधि को वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कुछ लोगों का मत है कि इनके लिए स्थान आरक्षित रखना समानता के विपरीत है। मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर वी०पी० सिंह की सरकार सामाजिक एवं शिक्षा के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केन्द्रीय सेवाओं के लिए नौकरियों में 28% स्थान सुरक्षित रखना चाहती थी, जिसके विरोध में भारत के अनेक युवकों को आत्मदाह करना पड़ा।
यह सरकार के लिए बहुत शर्म का विषय था। पी०वी० नरसिम्हा राव की सरकार ने सामाजिक एवं शिक्षा के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केन्द्रीय सेवाओं के लिए आर्थिक स्थिति और जोड़ने की घोषणा की। इसके साथ ही 10 प्रतिशत स्थान उनके लिए भी आरक्षित किए जाएँगे जो आर्थिक कारण से तो कमज़ोर हैं, लेकिन उच्च जातीय वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। अभी तक इस जटिल समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
12. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा विषयक परिकल्पना स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में अनेक अल्पसंख्यक वर्ग थे और आज भी पाए जाते हैं। अल्पसंख्यकों को धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुस्लिम अपने-आपको अल्पसंख्यक मानते थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुस्लिम संरक्षण की माँग की।
सरकार ने उनकी माँग को मान लिया और कानून द्वारा उनके हितों की रक्षा का प्रावधान किया। विभाजन के समय अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों के कारण संविधान सभा के सदस्य भयभीत थे और वे स्वतन्त्र भारत में इसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। इसलिए संवैधानिक सभा की एक समिति का गठन किया गया . जो भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा सम्बन्धी समस्या पर विचार करेगी।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। ऐंग्लो इण्डियन के लिए विधानपालिका में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। भाषा व संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएँ खोलने का अधिकार दिया गया है।
13. संयुक्त चुनाव-प्रणाली विषयक परिकल्पना-संविधान सभा के सदस्य स्वतन्त्रता से पूर्व प्रचलित साम्प्रदायिक चुनाव-प्रणाली के कुप्रभावों से अवगत थे। मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार को तथा हिन्दू मतदाता हिन्दू उम्मीदवार को वोट डालते थे। इस चुनाव-प्रणाली के आधार पर हिन्दुओं और मुसलमानों में घृणा की भावना पैदा हुई, जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हआ तथा पाकिस्तान राज्य की स्थापना हुई।
संविधान निर्माता इस प्रणाली को समाप्त करने के पक्ष में थे। भारतीय नवीन संविधान के द्वारा इस प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त चुनाव-प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अब भारत में सभी सम्प्रदाय मिल-जुलकर अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं।
14. विश्व शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की परिकल्पना संविधान सभा के सदस्य दो विश्वयुद्धों का कटु अनुभव अपने साथ लिए हुए थे जिसमें लाखों लोगों की जानें गई थीं। उनकी इच्छा थी कि फिर से धरती पर ऐसा युद्ध न हो। उधर वे जापान की युद्ध-त्याग की नीति से भी प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने विश्व-शान्ति व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने का संकल्प लिया।
नवीन भारतीय संविधान विश्व-शान्ति का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत राष्ट्रों के बीच न्याय तथा समानतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करेगा, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए विधि एवं सन्धि बन्धनों के प्रति आदर का भाव रखेगा और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। इस सन्दर्भ में पं० जवाहरलाल नेहरू जी की पंचशील नीति की सराहनीय भूमिका रही है। वास्तव में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष भूमिका निभाई है। आज विश्व की राजनीति में भारत का प्रमुख स्थान है।
निष्कर्ष-उपरोक्त परिकल्पनाओं व दृष्टिकोणों का विस्तृत अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में नवीन भारत की एक कल्पना थी जिसे वे कार्य रूप देना चाहते थे तथा उसी कल्पना के आधार पर उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण करते समय निर्माताओं ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि
ऐसा संविधान बने जिसे कार्यान्वित भी किया जा सके, क्योंकि कल्पनाओं व सपनों में बहकर कहीं ऐसा संविधान न बन जाए जो मात्र आदर्श बनकर रह जाए। अतः संविधान निर्माता वर्तमान संविधान में अपना उद्देश्य (जनता को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय) दिलवाने में सफल रहे।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छाँटकर लिखें
1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ निम्नलिखित शब्दों से होता है
(A) भारत एक समाजवाद……
(B) भारत के लोग……
(C) भारत को प्रभुसत्ता संपन्न
(D) हम भारत के लोग
उत्तर:
(D) हम भारत के लोग
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ तथा ‘धर्म-निरपेक्ष’ शब्द जोड़े गए
(A) 42वें संशोधन द्वारा
(B) 44वें संशोधन द्वारा
(C) 46वें संशोधन द्वारा
(D) 52वें संशोधन द्वारा
उत्तर:
(A) 42वें संशोधन द्वारा
3. भारतीय संविधान लागू हुआ
(A) 15 अगस्त, 1947 को
(B) 26 जनवरी, 1946 को
(C) 26 जनवरी, 1950 को
(D) 26 जनवरी, 1952 को
उत्तर:
(C) 26 जनवरी, 1950 को
4. भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं
(A) 395
(B) 238
(C) 138
(D) 295
उत्तर:
(A) 395

5. प्रस्तावना में वर्णन नहीं किया गया है
(A) प्रेस की स्वतंत्रता का
(B) पद और अवसर की समानता का
(C) विचारों की स्वतंत्रता का
(D) विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का
उत्तर:
(A) प्रेस की स्वतंत्रता का
6. प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं है?
(A) सामाजिक न्याय
(B) आर्थिक न्याय
(C) राजनीतिक न्याय
(D) धार्मिक न्याय
उत्तर:
(D) धार्मिक न्याय
7. प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है
(A) राष्ट्रपति द्वारा
(B) प्रधानमंत्री द्वारा
(C) संसद द्वारा
(D) राज्यपालों द्वारा
उत्तर:
(C) संसद द्वारा
8. प्रस्तावना में अब तक संवैधानिक विधि द्वारा संशोधन किया गया है
(A) दो बार
(B) चार बार
(C) एक बार
(D) तीन बार
उत्तर:
(C) एक बार
9. निम्नलिखित में कौन प्र में कौन प्रभुसत्ता संपन्न है?
(A) लोकसभा
(B) राष्ट्रपति
(C) जनता
(D) संविधान
उत्तर:
(C) जनता
10. संविधान में उद्देश्य का वर्णन करते हैं
(A) प्रस्तावना में
(B) मौलिक अधिकारों में
(C) संकटकालीन अनुच्छेदों में
(D) राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांतों में
उत्तर:
(A) प्रस्तावना में
11. प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है?
(A) सामाजिक न्याय का
(B) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का
(C) आर्थिक न्याय का
(D) धार्मिक न्याय का
उत्तर:
(B) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का
12. संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन-से उद्देश्य घोषित नहीं हैं?
(A) सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय
(B) विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
(C) व्यक्ति की गरिमा व अवसर की समानता
(D) इसमें तीन सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं
उत्तर:
(D) इसमें तीन सूचियाँ-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं
13. भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता का अर्थ है
(A) राज्य धर्म विरुद्ध है
(B) राज्य धार्मिक है
(C) राज्य अधार्मिक है
(D) राज्य का कोई राजधर्म नहीं है
उत्तर:
(D) राज्य का कोई राजधर्म नहीं है
14. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द ‘सेक्यूलर’ का अर्थ है
(A) सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता
(B) एकेश्वरवाद
(C) बहुदेववाद
(D) सभी धर्मों को अस्वीकृत
उत्तर:
(A) सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता
15. भारतीय संविधान के किस काम को उसकी ‘आत्मा’ की संज्ञा दी जाती है?
(A) मौलिक अधिकारों को
(B) राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों को
(C) संविधान की प्रस्तावना को
(D) अनुसूचियों को
उत्तर:
(C) संविधान की प्रस्तावना को
16. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है ‘We, the people of India’ इससे निम्नलिखित में से क्या अर्थ निकलता है?
(A) भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है
(B) संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(C) भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर:
(D) उपर्युक्त सभी
17. संविधान की प्रस्तावना में वर्णन मिलता है
(A) संविधान के मूल्यों का
(B) राष्ट्रपति की शक्तियों का
(C) नागरिकों के अधिकारों का
(D) नागरिकों के कर्त्तव्यों का
उत्तर:
(A) संविधान के मूल्यों का
18. भारत गणराज्य है
(A) लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण
(B) संघात्मक प्रणाली के कारण
(C) राज्याध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:
(A) लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें
1. किसी देश में संविधान के मूल्यांकन के क्या आधार होते हैं?
उत्तर:
संविधान में निहित उद्देश्य, आदर्श एवं मूल्य संविधान के मूल्यांकन का आधार होते हैं।
2. क्या प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग होती है?
उत्तर:
संविधान में निहित उद्देश्य, आदर्श एवं मूल्य संविधान के मूल्यांकन का आधार होते हैं।
3. क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है?
उत्तर:
हाँ।
4. भारतीय संविधान में मान्य सवैधानिक भाषाएँ कितनी हैं?
उत्तर:
22
5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारम्भ किन शब्दों से होता है?
उत्तर:
हम भारत के लोग ……….. शब्दों से होता है।
6. 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता के साथ कौन-सा शब्द और जोड़ा गया?
उत्तर:
अखण्डता।
7. भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान की किस धारा में किया गया है?
उत्तर:
368 में।
रिक्त स्थान भरें
1. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ………….. का प्रतीक है।
उत्तर:
गणराज्य
2. ……………. संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जोड़े गए।
उत्तर:
42वें

3. भारतीय संविधान में ……………. मान्य सवैधानिक भाषाएँ हैं।
उत्तर:
22
4. भारत में …………… नागरिकता दी गई है।
उत्तर:
इकहरी
5. ……………. सवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में आरक्षण की अवधि को सन 2030 तक बढ़ा दिया गया।
उत्तर:
104वें
6. भारत में ……………. निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है।
उत्तर:
संयुक्त
7. प्रस्तावना को संविधान की ……………. कहा जाता है।
उत्तर:
आत्मा
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()