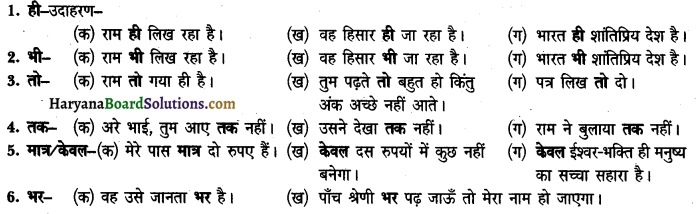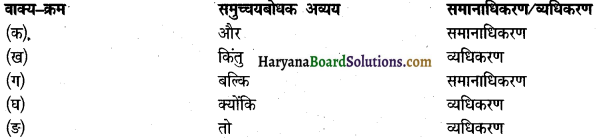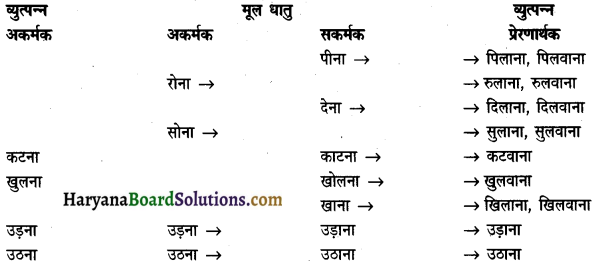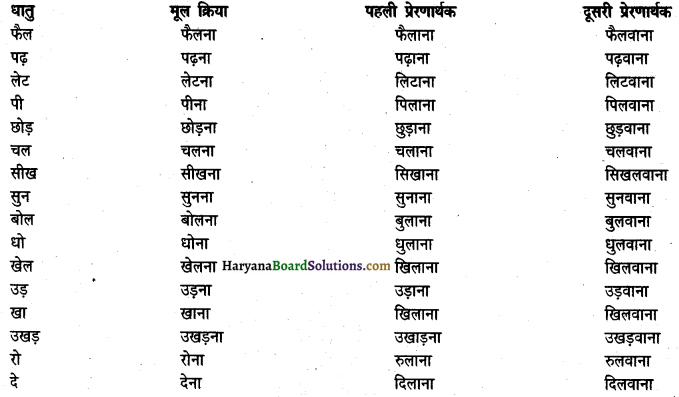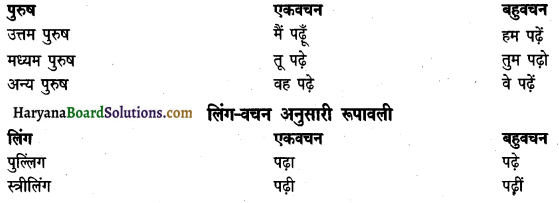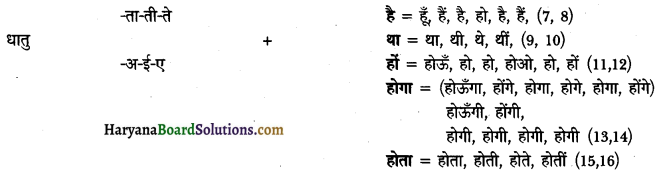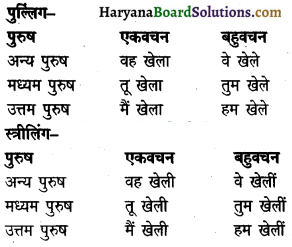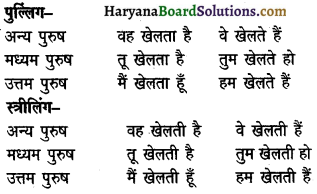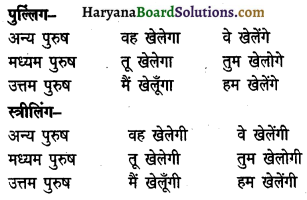Haryana State Board HBSE 10th Class Hindi Solutions Hindi Rachana Nibanbh-Lekhan निबंध-लेखन Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 10th Class Hindi Rachana निबंध-लेखन
रचना निबंध-लेखन HBSE 10th Class Hindi
निबंध-लेखन
1. हमारा प्यारा भारतवर्ष
संकेत : भूमिका, नामकरण, प्राचीन इतिहास, भारत-विविधताओं का देश, प्राकृतिक सौंदर्य, उपसंहार।
राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस भूमि के अन्न-जल से मानव का शरीर बनता है, विकसित होता है, उसके प्रति अनायास प्रेम, श्रद्धा तथा लगाव पैदा हो जाता है। सभी प्राणी अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं तथा जिससे प्यार किया जाता है, उसकी हर वस्तु में सौंदर्य नज़र आता है। हम भारतवासियों को भी अपने देश से प्रेम है, हमें यहाँ की हर वस्तु में सौंदर्य दिखाई देता है। यह देश इतना पवित्र तथा गरिमामय है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। अपनी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहा भी गया है
‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।’
हमारे देश का नाम ‘भारत’ या ‘भारतवर्ष’ है। पहले इसका नाम आर्यावर्त था। कुछ विद्वानों का मानना है कि दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। इसे ‘हिंदुस्तान’ भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे ‘इंडिया’ भी कहते हैं।
मेरा महान देश सब देशों में शिरोमणि है। आधुनिक उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम तक फैला है। प्रकृति ने इसकी देह को एक देवी का रूप दिया है। बर्फ की चोटियों से ढका हिमालय इसके सिर पर मुकुट के समान है। अटक से कटक तक इसकी बाँहें फैली हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी इसके चरण हैं, जिन्हें हिंद सदा धोता रहता है।
भारत का अतीत स्वर्णिम रहा है। एक समय था, जब यह सोने की चिड़िया कहलाता था। यह देश धन-धान्य तथा सौंदर्य से विभूषित था। इसी देश ने ज्ञान की किरणें पूरे विश्व में फैलाईं। इस देश पर मुसलमानों, मुगलों और अंग्रेज़ों ने आक्रमण करके यहाँ अपना राज्य स्थापित किया और इसे लूटा। पर हमारे देश के वीर सैनिकों व क्रांतिकारियों ने 15 अगस्त, 1947 को देश को स्वतंत्र करवाया और आज हमारा भारत हर क्षेत्र में उन्नत और शक्तिशाली होता जा रहा है।
भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं और समुद्र भी हैं, हरियाली भी है, तो रेगिस्तान भी हैं। यहाँ गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत हर प्रकार के मौसम हैं। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं- सिक्ख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम आदि। यहाँ मंदिर, मस्ज़िद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी हैं। यहाँ अनेक भाषाएँ हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, उर्दू, मलयालम आदि बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, धर्म तथा विचारों आदि में विविधता है। परंतु सभी भारतवासी एक परिवार के समान रहते हैं और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना में विश्वास करते हैं। यह विविधता ही भारत की शान है और हमारी उन्नति का कारण है।
भारत का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ एक ओर कश्मीर में धरती का स्वर्ग दिखलाई पड़ता है, तो दूसरी ओर केरल की हरियाली आनंद देने वाली तथा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ सभी ऋतुएँ समय पर आती हैं तथा अपनी विविध विशेषताओं से धरती को अनूठी छटा से भर देती हैं। इस देश की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कवि रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है-
शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक
गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जयगीतों से अब तक
भारत अत्यंत प्राचीन देश है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने विश्व को सत्य, अहिंसा तथा सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ाया। ज्ञान के क्षेत्र में सारा विश्व भारत का ऋणी है। इसी पर विज्ञान का ढाँचा टिका हुआ है। ज्ञान का भंडार होने के कारण भारत को ‘जगद्गुरु’ तथा धन-वैभव के कारण ‘सोने की चिड़िया’ कहा गया।
आज भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्म-निर्भर है। देश में उद्योग-धंधों का जाल-सा विछा हुआ है और विश्व के विकासशील देशों में अग्रणी स्थान प्राप्त है। परंतु दुर्भाग्य से हर प्रकार की संपन्नता होकर पर भी भारत का वर्तमान निराशा से भरपूर है। आज भारत में धर्म, भाषा तथा जाति के आधार पर झगड़े होते रहते हैं। भ्रष्टाचार ने चारों ओर अपने पाँव पसार लिए हैं। महँगाई आसमान को छू रही है। इस प्रकार मेरा देश भारत अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। हम सभी का कर्तव्य है कि देश को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में अपना योगदान दें, जिससे देश अपना गौरव फिर से प्राप्त कर सके।

रचना निबंध-लेखन 10th Class Hindi HBSE
2. नोटबन्दी का एक वर्ष
नोटबंदी’ का अर्थ है कि जब पुराने नोट बंद कर दिए जाएँ और उनके स्थान पर नए नोटों का प्रचलन हो। नोटबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरानी मुद्रा को कानूनन प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है और उसके बदले नई मुद्रा या नोट छाप दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से जब नए नोट समाज में आ जाते हैं तो पुराने नोटों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। पुराने नोटों को बैंकों में बदलवाया जा सकता है। नोटों को बदलवाने के लिए भी समय निर्धारित किया जाता है।
नोटबंदी करना क्यों आवश्यक होता है? वस्तुतः समाज में भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, महँगाई व आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए नोटबंदी की जाती है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नोटबंदी से ऐसा धन पकड़ा जाता है। नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए भी नोटबंदी करना अनिवार्य हो जाता है।
भारतवर्ष कोई अकेला ऐसा देश नहीं जहाँ नोटबंदी लागू की गई हो। यूरोप में भी यूरो नाम की नई करेंसी चलाई गई थी। तब पुराने नोट बैंकों में जमा करवा दिए गए थे। यूरोप में इस नोटबंदी से बहुत बड़ा बवाल मचा था। जिम्बाब्बे में भी महंगाई पर लगाम कसने के लिए सन् 2014 में नोटबंदी का प्रयोग किया गया था।
भारतवर्ष में भी यह कोई प्रथम बार नोटबंदी नहीं थी। इससे पूर्व भी यहाँ कई बार नोटबंदी हो चुकी है। भारत में प्रथम बार सन् 1946 में 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों की नोटबंदी की गई थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में भी नोटबंदी हुई थी। भारत में 2005 ई० में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 500 रुपए के नोटों को बदला था। इसके अतिरिक्त छोटे सिक्कों का प्रचलन भी अब नहीं होता। उन्हें भी अब बंद कर दिया गया है।
सन् 2016 की 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी की कहानी ही अलग है, क्योंकि इन दो करेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86% भाग को अपने कब्जे में किया हुआ था। बाज़ार में इन्हीं नोटों का अधिक प्रचलन होता था।
8 नवम्बर, 2016 को जब रात्रि 8:15 पर घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कुछ घोषणाएँ करने जा रहे हैं तो लोगों को उम्मीद थी कि भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाली नोक-झोंक सम्बन्धी कोई नई घोषणा करेंगे। किन्तु उन्होंने 500 और 1000 रुपए नोटों की नोटबंदी करके सबको हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुईं। कुछ लोग प्रधानमंत्री की नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो कुछ विरोध। कुछ तो इस नोटबंदी को खारिज करवाने के लिए सड़कों पर भी उतर आए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी के अगले दिन ही बैंकों में नोट बदलवाने के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लग गई थी। नोट बदलवाने के लिए नियमों को भी सख्ती से लागू किया गया। सरकार ने अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए केवल 50 दिन का समय माँगा था। पुराने नोटों के स्थान पर पाँच सौ और दो हज़ार के नए नोटों को चलाया गया।
नोटबंदी के समय मीडिया की भूमिका भी सराहनीय रही। मीडिया के कुछ लोगों ने नोटबंदी की सराहना की तो कुछ ने इसका विरोध करते हुए अनेक तर्क-वितर्क प्रस्तुत किए।
नोटबंदी केवल शोर मचाने के लिए नहीं की जाती। हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि नोटबंदी के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। नोटबंदी से काले धन पर नियन्त्रण किया जा सकता है। महँगाई की दर घटाई जा सकती है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है। इन सबके अतिरिक्त जनता में आर्थिक जागरूकता का विकास होता है। किन्तु इसे लागू करने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नोटबंदी के कारण ही लोगों में आर्थिक कर व उसके प्रति जिम्मेवारी का अहसास हुआ। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि ऑनलाइन व डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला। छोटे-छोटे दुकानदारों ने भी अब ऑनलाइन भुगतान करवाना आरम्भ कर दिया है।
कुछ लोगों का विचार है कि नोटबंदी से आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, किन्तु भविष्य में इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। नोटबंदी के कारण ही नकली नोट छपने बंद हो गए। काले धन को समाप्त करने के लिए भी यह नोटबंदी कारगर सिद्ध हुई है। नोटबंदी के कारण ही कैशलैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।
नोटबंदी पर विचार करते समय जहाँ उसके अनेक लाभ नज़र आए, वहीं उसकी हानियाँ भी दिखाई दीं। नोटबंदी से सबसे बड़ी हानि यह हुई कि साधारण जनता की दैनिक जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आईं। जनता को बैंकों व ए०टी०एम० के सामने घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था। अस्पताल का बिल, बिजली का बिल, किराए की समस्या आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किन्तु ये सब कठिनाइयाँ बहुत अस्थाई व तात्कालिक थीं। कुछ समय के पश्चात् सब कुछ सामान्य हो गया।
इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय जनता ने नोटबंदी का स्वागत किया तथा सरकार की सराहना भी की। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारत के इस निर्णय का स्वागत किया गया। निश्चय ही नोटबंदी से कुछ सीमा तक भारत में भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। कुछ लोगों ने अपना काला धन सरकार को समर्पण भी कर दिया। इस दिशा में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सार रूप में कहा जा सकता है कि सन् 2016 का नोटबंदी का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध हुआ है। यदि भारत को विकास के पथ पर अग्रसर रहना है तो ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। हर कार्य के गुण व अवगुण दोनों ही होते हैं। अच्छी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हिम्मत का कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसे कदम के लिए देश की जनता का भरोसा व हौंसला भी बहुत बड़ी बात होती है। अतः जनता को इस कार्य में सरकार की मदद करनी चाहिए। बड़ी-बड़ी योजनाओं को लागू करने व बड़े-बड़े निर्णय लेने के लिए देश, जनता और सरकार को मिलकर कार्य करना पड़ेगा।

3. राष्ट्रीय एकता
संकेत : भूमिका, भारत में उत्पन्न समस्याएँ, दूषित राजनीति, असमानताओं में समानता, उपसंहार।
किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत-से लोगों का मिलकर कार्य करना संगठन कहलाता है। संगठन ही सभी शक्तियों की जड़ है। एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, एकता एक महान् शक्ति है। एकता के बल पर ही छोटे-से-छोटा व्यक्ति भी अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। जिस परिवार में एकता होती है, वहाँ सदा सुख-समृद्धि एवं शांति रहती है। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। छोटे-छोटे जीव-जंतु भी संगठन के बल पर अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेते हैं। मधुमक्खियाँ एकत्रित होकर एक बहुत बड़े रस के पिंड का निर्माण कर लेती हैं।
अल्पानामापि वस्तूनाम संहाति कार्यसाधिका।
तृण गुणत्वमान्नैः वध्यन्ते मत्त हस्तिनः।।
अर्थात् छोटी-छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। जैसे छोटे-छोटे तृण रस्सी के रूप में परिणित हो जाते हैं तो उससे मतवाले हाथी भी बाँधे जा सकते हैं। एकता वह शक्ति है, जिसके बिना कोई भी देश, समाज तथा संप्रदाय उन्नति नहीं कर सकता। एकता के अभाव के कारण ही हम लोग सैकड़ों वर्ष अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। हमारी कमज़ोरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने मनमाने अत्याचार किए, भारत की संस्कृति पर कुठाराघात किए। उन लोगों ने हमारी मान-मर्यादाएँ लूटीं और हम परतंत्रता की बेड़ियों में इस प्रकार जकड़ गए कि उनसे मुक्ति की कल्पना ही संदिग्ध प्रतीत होने लगी।
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से ही भारत में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती रही हैं। इनमें सांप्रदायिक समस्या प्रमुख है। हमारे देश का विभाजन भी इसी समस्या के आधार पर हुआ। कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने देश में सांप्रदायिकता की आग फैला दी, जिससे हम आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। वर्तमान देश में अनुशासन तथा आपसी सहयोग के वातावरण की अति आवश्यकता है।
कुछ वर्षों से हमारे देश में दूषित राजनीति से विषैला वातावरण बनता जा रहा है। धर्मांधता के कारण लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अपने-अपने स्वार्थों में लिप्त लोग आपसी प्रेम को भूल रहे हैं। स्वार्थ की भावनाओं, प्रांतीयता एवं भाषावाद के कारण राष्ट्रीय भावना प्रभावित हुई है। हमारे देश के लोगों में संकीर्णता की भावना पनप रही है और व्यापक दृष्टिकोण लुप्त होता जा रहा है। इसलिए विश्व-बंधुत्व की भावना अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है। अगर किसी ने प्रयास भी किया तो वह प्रदेश स्तर तक ही जाकर असफल हो गया। इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर, असम आदि प्रदेशों में नर-संहार के किस्से सुनने को मिलते हैं। इन सबके लिए वे स्वार्थी नेता ज़िम्मेदार हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश को दाँव पर लगा रहे हैं। अनेक विषमताओं के होते हुए भी जब हम राष्ट्रीय एकता के विषय में विचार करते हैं तो पता चलता है कि इस राष्ट्रीय एकता के कारण धार्मिक भावना, आध्यात्मिकता, समन्वय की भावना, दार्शनिक दृष्टिकोण, साहित्य, संगीत और नृत्य आदि अनेक ऐसे तत्त्व हैं, जो देश को एकता के सूत्र में बाँधे हुए हैं। बस सरकार और जनता को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आज राष्ट्रीय एकता के लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का प्रबंध करना आवश्यक है।
शत्रुपक्ष पर कठोर दंडनीति लागू की जाए। पुलिस की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जाए। आज सभी संगठनों को मिलकर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता राष्ट्रीय एकता पर आधारित है। इसके अभाव में हमारी स्वतंत्रता भी असंभव है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें भरपूर प्रयत्न करने चाहिएँ, एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे हम और हमारे वंशज स्वतंत्रता की खुली हवा में साँस लेते रहें। यद्यपि विघटन की प्रवृत्ति हमें झकझोर देती है और राष्ट्रीय एकता को संकट-सा प्रतीत होने लगता है, परंतु देश की आत्मा बलपूर्वक एकरूपता को प्रकट कर देती है।
हर्ष की बात है कि आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्र की आय का तीन प्रतिशत व्यय कर रहा है और हमारी भारत सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हम अपने देशवासियों से यह निवेदन कर रहे हैं कि वे अपने पूर्वजों के समान ही एकता के सूत्र में बँध जाएँ, क्योंकि सही अर्थ में देश की उन्नति ही आपकी अपनी उन्नति है।

4. स्वदेश-प्रेम
संकेत : भूमिका, देशप्रेम एक स्वाभाविक गुण, भारतवर्ष प्यारा देश, देश के प्रति हमारा कर्त्तव्य, भारत एक विशाल देश, उपसंहार।
देशभक्ति पावन गंगा नदी के समान है जिसमें स्नान करने से मनुष्य ही नहीं, अपितु उसका मन और अंतरात्मा भी पावन हो जाती है। स्वदेश-प्रेम का अर्थ है-अपने देश या वतन की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए अपना तन, मन और धन देश के चरणों में सौंप देना। जिस देश की धूलि में लोट-लोटकर हम बड़े हुए हैं तथा जिसके अन्न, जल और वायु का सेवन करके हम विकसित हुए हैं, उसकी सेवा न करना कृतघ्नता है। वस्तुतः माता और मातृभूमि के ऋण से आदमी आजीवन मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान राम ने सोने की लंका देखकर लक्ष्मण से कहा था-जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
मनुष्य में अपने देश के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। मनुष्य ही क्यों, पशु-पक्षियों में भी यह गुण देखा जा सकता है। पक्षी दूर दिशाओं से उड़कर शाम को अपने घोंसलों में लौट आते हैं। गाँव से दूर वनों में चरने वाले गाय-भैंस आदि पशु भी दिन छिपते ही अपने खूटों पर पहुँचकर सुख-शांति प्राप्त करते हैं। इसके पीछे एक कारण है-अपने स्थान से प्रेम। इसी प्रकार, मनुष्य चाहे किसी भी काम से विदेश में रहता हो परंतु उसके हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम ज्यों-का-त्यों बना रहता है। वह अपने देश, घर और परिवार को याद करता है परंतु जिस व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं है वह तो पशुओं से भी निकृष्ट है। ऐसा व्यक्ति जीवन में तो अपयश प्राप्त करता ही है, मर कर भी नरक भोगता है।
हिमालय के विशाल आँगन में विद्यमान हमारा भारतवर्ष प्रिय देश है। भारत-भूमि पर ही सबसे पहले मानव सभ्यता और संस्कृति का आरंभ हुआ। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने ही ज्ञान प्राप्त किया। हमने ही संसार को यह ज्ञान दिया। हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध जैसे अवतार हुए जिन्होंने संसार को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध और अशोक ने यह सिद्ध कर दिखाया कि विजय केवल शस्त्रों से ही नहीं, अपितु सत्य और अहिंसा से भी प्राप्त की जा सकती है। हमारे देश के पर्वत, नदियाँ, सागर, हरे-भरे जंगल, खेत-खलिहान सब कुछ हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम-भावना उत्पन्न करते हैं। कविवर प्रसाद ने सही कहा है-
जिएँ तो सदा उसके लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष।
निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ।।
आज हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र है। अतः स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देशभक्तों का कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया है। हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। हमारे किसान और मज़दूर बहुत गरीब तथा पिछड़े हुए हैं। हमारे गाँवों में अभी भी पिछड़ापन है। हमें उनकी स्थिति को सुधारना है। असहाय और बेरोज़गारों को रोज़गार देना है। सबके लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था करनी है। करोड़ों अनपढ़ों को पढ़ाना है। संसार के विकसित देशों को शोषण से बचाने के लिए हमें अधिकाधिक उद्योगों का विकास करना है। यद्यपि हमारी सरकार इस दिशा में अनेक प्रयत्न कर रही है, लेकिन वे प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं। आज ऐसे देशभक्तों की आवश्यकता है जो अपना तन, मन और धन सभी कुछ देश के चरणों में अर्पित कर दें।
हमारा भारत एक विशाल देश है। इसकी जनसंख्या एक अरब से भी अधिक पहुँच चुकी है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हमने धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की। हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कभी-कभी हममें विचारों की भिन्नता भी पैदा हो जाती है। यहाँ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल तथा तेलुगू आदि अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। कभी-कभी यह भाषा-मोह हमारे अंदर आपसी भेदभाव उत्पन्न कर देता है परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमारा अपना देश है। हमारा जन्म यहीं हुआ है। हमारे आपसी झगड़े इसे कमज़ोर बना सकते हैं। अतः हमें परस्पर स्नेह और प्रेम के साथ रहना चाहिए। उर्दू के कवि इकबाल साहब ने ठीक कहा है-
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।।
हमारी संस्कृति का मूल-मंत्र भी यही है। जो लोग धर्म के नाम पर घृणा, वैर-भाव और ईर्ष्या-द्वेष फैलाते हैं, वे सच्चे भारतवासी नहीं हैं। ऐसे लोग निश्चय ही देशद्रोही हैं।
देश की उन्नति के लिए भी स्वदेश-प्रेम आवश्यक है। जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में ही अपना कल्याण समझते हैं और देश के विकास में अपना विकास-वे अन्य देशों के सामने अपने देश का नाम ऊँचा करते हैं। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति भी देशभक्त देशवासियों पर निर्भर करती है। जिन देशों के बालक, वृद्ध, स्त्रियाँ, युवक अपने देश की बलिवेदी पर अपने स्वार्थों को न्योछावर करते हैं, वे देश ही संसार में शक्तिशाली देश समझे जाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में निःस्वार्थ देशभक्तों की कमी है। यही कारण है कि हमारा देश अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाया। अतः हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए देशप्रेम की भावना का विकास करना चाहिए।

5. राष्ट्रभाषा हिंदी
सकेत : भूमिका, अंग्रेज़ी-हिंदी का विवाद, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, हिंदी के विकास के प्रयत्न, हिंदी का विरोध, हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में समर्थ, उपसंहार।
‘राष्ट्र’ शब्द का प्रयोग किसी देश तथा वहाँ बसने वाले लोगों के लिए किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उसमें विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न स्थानों अथवा प्रांतों में रहने वाले लोगों की भाषा भी अलग-अलग होती है। इस भिन्नता के साथ-साथ उनमें एकता भी बनी रहती है। पूरे राष्ट्र के शासन का एक केंद्र होता है। अतः राष्ट्र की एकता को और दृढ़ बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी व्यापक भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतवर्ष में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतवर्ष को यदि भाषाओं का अजायबघर भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी लेकिन एक संपर्क भाषा के बिना आज पूरे राष्ट्र का काम नहीं चल सकता।
सन 1947 में भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जब तक भारत में अंग्रेज़ शासक रहे, तब तक अंग्रेज़ी का बोलबाला था किंतु अंग्रेजों के जाने के बाद यह असंभव था कि देश के सारे कार्य अंग्रेज़ी में हों। जब देश के संविधान का निर्माण किया गया तो यह प्रश्न भी उपस्थित हुआ कि राष्ट्र की भाषा कौन-सी होगी ? क्योंकि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र के स्वतंत्र अस्तित्व की पहचान नहीं होगी। कुछ लोग अंग्रेज़ी भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाए रखने के पक्ष में थे परंतु अंग्रेज़ी को राष्ट्रभाषा इसलिए घोषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि देश में बहुत कम लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ी बोल सकते थे। दूसरे, उनकी भाषा को यहाँ बनाए रखने का तात्पर्य यह था कि हम किसी-न-किसी रूप में उनकी दासता में फँसे रहें।
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रमुख तर्क यह है कि हिंदी एक भारतीय भाषा है। दूसरे, जितनी संख्या यहाँ हिंदी बोलने वाले लोगों की थीं, उतनी किसी अन्य प्रांतीय भाषा बोलने वालों की नहीं। तीसरे, हिंदी समझना बहुत आसान है। देश के प्रत्येक अंचल में हिंदी सरलता से समझी जाती है, भले ही इसे बोल न सकें। चौथी बात यह है कि हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है, इसमें शब्दों का प्रयोग तर्कपूर्ण है। यह भाषा दो-तीन महीनों के अल्प समय में ही सीखी जा सकती है। इन सभी विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि बनाया जाए।
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के बाद उसका एकदम प्रयोग करना कठिन था। अतः राजकीय कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई थी कि सन 1965 तक केंद्रीय शासन का कार्य व्यावहारिक रूप से अंग्रेज़ी में चलता रहे और पंद्रह वर्षों में हिंदी को पूर्ण समृद्धिशाली बनाने के लिए प्रयत्न किए जाएँ। इस बीच सरकारी कर्मचारी भी हिंदी सीख लें। कर्मचारियों को हिंदी पढ़ने की विशेष सुविधाएँ दी गईं। शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य विषय बना दिया गया।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिंदी के पारिभाषिक शब्द-निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ हिंदी को दी गईं ताकि हिंदी, अंग्रेज़ी का स्थान पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले। अनेक भाषा-विशेषज्ञों की राय में यदि भारतीय भाषाओं की लिपि को देवनागरी स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रीय भावात्मक एकता स्थापित करने में सुविधा होगी। सभी भारतीय एक-दूसरे की भाषा में रचे हुए साहित्य का रसास्वादन कर सकेंगे।
आज जहाँ शासन और जनता हिंदी को आगे बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए प्रयत्नशील हैं वहाँ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उसको टाँग पकड़कर पीछे घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी को संविधान के अनुसार सरकारी भाषा बनाने से तो सहमत हैं किंतु उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे भी हैं जो उर्दू का निर्मूल पक्ष में समर्थन करके राज्य-कार्य में विघ्न डालते रहते हैं। धीरे-धीरे पंजाब, बंगाल और चेन्नई के निवासी भी प्रांतीयता की संकीर्णता में फँसकर अपनी-अपनी भाषाओं की मांग कर रहे हैं परंतु हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
निःसंदेह हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें राष्ट्रभाषा बनने की पूर्ण क्षमता है। इसका समृद्ध साहित्य और इसके प्रतिभा संपन्न साहित्यकार इसे समूचे देश की संपर्क भाषा का दर्जा देते हैं किंतु आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हिंदी का प्रचार-प्रसार कैसे किया जाए ? सर्वप्रथम तो हिंदी भाषा को रोज़गार से जोड़ा जाए। हिंदी सीखने वालों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए। वहाँ हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों एवं संपादकों को और आर्थिक अनुदान दिया जाए।
आज हिंदी के प्रचार-प्रसार में कुछ बाधाएँ अवश्य हैं किंतु दूसरी ओर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें एवं जनता सभी एकजुट होकर हिंदी के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में सरकारी कामकाज हिंदी में किया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी हिंदी में कार्य करना आरंभ कर दिया है। विभिन्न संस्थाओं एवं अकादमियों द्वारा हिंदी लेखकों की श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा भी इस दिशा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं।
6. दीपावली पर पटाखों का प्रदूषण
दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सुप्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण त्योहार है। इसका धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक महत्त्व भी अत्यधिक है। यह केवल हिन्दुओं का त्योहार ही नहीं है, अपितु देश के हर धर्म के लोग इसे मनाते हैं। ‘दीपावली’ का अर्थ होता है-दीपों की पंक्ति। इस त्योहार पर लोग अपने घरों को दीपों के द्वारा सजाते हैं। इसलिए इसे ‘प्रकाश का त्योहार’ भी कहा जाता है। इस त्योहार को श्रीराम के चौदह वर्ष का बनवास काटकर अयोध्या लौटने की खुशी में मनाते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है।।
निश्चय ही यह त्योहार खुशियों का त्योहार है, किन्तु इस त्योहार के मनाने में अब कुछ बुराइयाँ भी सम्मिलित हो गई हैं; जैसे जुआ खेलना, शराब आदि का सेवन करना तथा अत्यधिक पटाखों का जलाना आदि। आजकल पटाखे इतनी अधिक मात्रा में जलाए जाते हैं कि जिससे इस त्योहार का सारा महत्त्व समाप्त हो जाता है।
पटाखों के चलाने से पर्यावरण प्रदूषण में कई गुणा वृद्धि होती है। प्रदूषण की समस्या पहले ही विश्व के लोगों के लिए एक बहुत गम्भीर समस्या बनी हुई है। आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण अपनी चरमसीमा को छू रहा है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लग रही है। भारतवर्ष में पटाखों के अत्यधिक प्रयोग के कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की मात्रा कई गुणा बढ़ जाती है। कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों से पहले ही वायु प्रदूषित होती है।
दीपावली के अवसर पर पटाखे जलाने से उनमें से निकलने वाली जहरीली गैस से वायु इतनी प्रदूषित हो जाती है कि साँस लेना भी दूभर हो जाता है। चारों ओर पटाखों से निकलने वाला धुआं फैल जाता है। इससे आँखों में जलन होने लगती है। फेफड़ों में जहरीले धुएं के पहुंचने से कई प्रकार की बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों का रक्तचाप भी बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पटाखों से निकलने वाली गैसों व धुएँ के कारण खुशियों का त्योहार मानव-जीवन के खतरे का त्योहार बनता जा रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान से कई प्रकार के दुष्परिणाम सामने आए हैं। पटाखों से निकलने वाले धुएँ एवं गैसों का मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
पटाखों के अन्धा-धुंध जलाने से अनेक दुर्घटनाएँ भी होती हैं। पटाखों के लापरवाही से चलाने पर बच्चों के हाथ-पैर जल जाते हैं। दूर जाकर गिरने वाली आतिशबाजी से आग लगने का भय भी बना रहता है। पटाखों के अवशेष भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
दीपावली के अवसर पर पटाखों के जलाने से ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। कई पटाखों से इतनी ध्वनि निकलती है कि कान के परदों के फटने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण कई बीमारियों के उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जाती है। अधिक ध्वनि के कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तनाव व बेचैनी भी बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन एवं फेफड़ों सम्बन्धी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वभाव पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने का भाव है कि दीपावली के त्योहार का प्रदूषण के कारण मजा किरकिरा हो जाता है।
यदि हम चाहते हैं कि दीपावली के त्योहार को मनाने का सही आनन्द प्राप्त करें तो हमें पटाखों के जलाने पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगानी होगी। उसे सहज भाव व सही ढंग से मनाना होगा। भारत सरकार ने पिछले वर्ष से पटाखों के जलाने से होने वाली दुर्घटनाओं और वायु व ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। पटाखों की बजाए दीप जलाने व फुल-झड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। पटाखों के जलाने से होने वाली हानियों के प्रति समाज में जागरूकता भी लानी चाहिए तभी इस बुराई से छुटकारा मिल सकता है। परम्परागत तरीकों से दीपावली का त्योहार मनाने से उसके वास्तविक महत्त्व का सन्देश जनता में जाएगा। हमें स्वयं अपने पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता को ध्यान में रखते हुए दीपावली पर न तो स्वयं पटाखे जलाने चाहिएँ और दूसरों को भी पटाखे न जलाने की प्रेरणा देनी चाहिए। तभी हम समाज में सौहार्द्रपूर्ण, स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण में दीपावली के त्योहार का सही आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।

7. स्वतंत्रता दिवस
संकेत : भूमिका, पराधीनता एक अभिशाप, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता दिवस का समारोह, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के प्रयास, उपसंहार।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार है। संसार में सभी प्राणी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि पिंजरे में बंद पक्षी भी स्वतंत्रता के लिए निरंतर अपने पंख फड़फड़ाता रहता है। उसे सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी में रखा स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता। वह भी स्वतंत्र होकर मुक्त गगन में स्वच्छंद उड़ान भरना चाहता है, फिर मनुष्य तो मनुष्य है। उसे भी स्वतंत्रता प्रिय है। वह भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता हुआ प्राणों की बाजी लगा देता है। महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है
‘पराधीन सपनेहुँ सुख नाही’। स्वतंत्रता जीवन और परतंत्रता मृत्यु के समान है। जब कोई राष्ट्र दुर्भाग्यवश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाता है, तो उसका जीवन अभिशाप बन जाता है। भारत जैसा महान् देश भी आपसी फूट और वैरभाव के कारण सैकड़ों वर्षों तक पराधीनता के अभिशाप को सहता रहा। पराधीनता के इतने लंबे दौर में हम घुन खाई हुई लकड़ी के समान कमज़ोर हो गए और अपनी संस्कृति तथा परंपराओं को भूलने लगे।
भारत की स्वतंत्रता की कहानी भी लगातार संघर्षों और बलिदानों की कहानी है। स्वतंत्रता की यह चिंगारी सन् 1857 में सुलगी थी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई, ताँत्या टोपे, नाना साहब आदि ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। स्वतंत्रता की यह चिंगारी भीतर-ही-भीतर भारतीयों के हृदय में निरंतर सुलगती रही। महात्मा गांधी, पं० नेहरू, लोकमान्य तिलक, सरदार पटेल, नेता जी सुभाष चंद्र बोस आदि ने स्वतंत्रता की इस चिंगारी को शोला बना दिया। भगतसिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ने इसे हवा दी। हम स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करते रहे। देशभक्तों ने जेलयात्राएँ की, लाठियाँ और गोलियाँ खाईं। अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंत में 1942 ई० में गांधी जी के नेतृत्व में ‘अंग्रेज़ो भारत छोड़ो’ का नारा लगाया। इस आंदोलन में बहुत-से भारतीयों ने भाग लिया।
परिणामस्वरूप अंग्रेज़ हिल गए। उन्होंने 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। इसी कारण प्रतिवर्ष 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह भारत की राजधानी दिल्ली में लालकिले पर मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देते हैं। दिल्ली में लालकिले पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं। रात्रि को सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व केवल भाषण देने या सुनने के लिए नहीं है। यह उन अमर शहीदों के बलिदानों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपना जीवन देकर हमें आज़ादी का उपहार दिया। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें आपसी भेदभाव, ऊँच-नीच को भुलाते हुए देश की उन्नति में अपने तन-मन-धन से सहयोग करना चाहिए।
‘अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ लुटा सकते नहीं।
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।’
इतने वर्षों से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। भाषा, धर्म, जाति, प्रांत आदि के नाम पर आज भी आपस में लड़ते-झगड़ते हैं। राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के ‘रामराज्य’ का सपना साकार नहीं हो पाया है। केवल भारतीय नवयुवक ही अब उस सपने को पूरा कर सकते हैं। आज देश की सीमाओं पर शत्रु अपनी आँख गड़ाए हुए हैं। हमें इसके लिए सचेत रहना चाहिए। हमें राष्ट्रीय एकता को और मज़बूत करना होगा, ताकि शत्रु अपने नापाक इरादों में सफल न हो सकें।
यह राष्ट्रीय पर्व हमें प्रतिवर्ष स्वतंत्रता के संघर्ष और उसमें शहीद होने वालों की याद दिलाता है। यह हमें स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा की शपथ लेता है।
8. भारतीय किसान
भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। कृषि ही यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। देश की कुल श्रम-शक्ति का लगभग 55 प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे सम्बन्धित उद्योग-धन्धों से अपनी आजीविका कमाता है। प्राचीनकाल में कृषक अपनी खेती-बाड़ी के काम से सन्तुष्ट था। कृषि अर्थात् खेती के साथ-साथ पशुओं को भी अपना धन मानता था। किन्तु मुस्लिम शासकों के समय में भारतीय किसान को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारतीय कृषक अंग्रेज़ों और जमींदारों के तरह-तरह के जुल्मों का शिकार हुआ। उसका जीवन जीना ही कठिन हो गया था।
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय किसान की दशा में कुछ सुधार हुआ। किन्तु जिस प्रकार कृषकों के शहरों की ओर पलायन करने एवं उनकी आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती हैं, उससे पता चलता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कोई भी किसान अपने बेटों को कृषक नहीं बनाना चाहता है। अन्नदाता कहलाने वाले कृषक की यह दशा हो जाना निश्चय ही चिंता का विषय है।
‘अन्नदाता’ व ‘सृष्टि पालक’ कहलाने वाला कृषक बहुत ही सरल और सहज जीवन व्यतीत करता रहा है। उसके पास किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। उसके जीवन की आवश्यकताएँ भी बहुत कम थीं। वह साधारण भोजन खाकर भी स्वर्ग के सुख की अनुभूति करता था। कठोर परिश्रम करने पर भी उसके जीवन की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। आज के किसान को घटते भू-क्षेत्र के कारण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, वर्षा हर समय उसे मेहनत करनी पड़ती है। इसके बावजूद उसे फसलों से उचित आय प्राप्त नहीं हो सकती।
कृषि संबंधी उपकरण, बिजली, बीज, खाद आदि महँगे होने के कारण कृषक का जीवन-स्तर और भी निम्न हुआ है। भारतीय कृषकों की गरीबी का अन्य प्रमुख कारण है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता के कारण प्रायः किसानों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी सूखे की मार पड़ती है तो कभी बाढ़ में सब कुछ बह जाता है। कृषि में श्रमिकों की साल भर आवश्यकता नहीं होती। इसलिए साल में कई मास उनको खाली बैठना पड़ता है। कृषकों के शहरों की ओर पलायन का यह भी एक बड़ा कारण है।
स्वतन्त्रता के पश्चात् कृषकों के सुधार के लिए अनेक आयोगों व कमेटियों का गठन किया गया तथा उन्हें कृषकों के जीवन-सुधार के अनेक सुझाव दिए गए। फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की भी घोषणाएँ की गईं किन्तु समय पर कभी भी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ।
कृषक की गरीबी का एक प्रमुख कारण उसकी अनपढ़ता भी रहा है। प्रायः यह देखा गया है कि अनपढ़ता के कारण ही कृषकों को खेती के नए-नए तरीके एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में उचित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण फसलों से उचित लाभ नहीं मिल सकता। इस दिशा में भारत सरकार ने यद्यपि कई कदम उठाए हैं, जैसे किसान कॉल सेन्टर, इससे बिना कोई शुल्क दिए कृषक अपने खेती के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेडियो व टी०वी० पर भी कृषि चैनलों की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरल नॉलेज सेन्टर्स की भी स्थापना की है। इन केन्द्रों पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी व दूर संचार तकनीक का उपयोग किसानों को वांछित जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
भारत सरकार ने किसानों को खाली समय में काम देने के लिए राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी योजना का 2006 में शुभारम्भ किया। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम-से-कम 100 दिन के ऐसे रोजगार की गारण्टी देता है। इस योजना में 33 प्रतिशत लाभ महिलाओं को दिया जाता है।
आज का कृषक यद्यपि पहले की अपेक्षा बहुत जागरूक हो चुका है। वह आज संगठन बनाकर अपनी जरूरी माँगों को सशक्त रूप से सरकार के सामने रखता है और आन्दोलन करता है। फिर भी अनपढ़ता, अन्धविश्वास और कई व्यसनों में फंसा होने के कारण उसकी आर्थिक दशा में मनोवांछित सुधार नहीं हो सका। आज भी वह शोषण का शिकार बना हुआ है। उसके परिश्रम का फल व्यापारी वर्ग लूट ले जाता है। उसकी मेहनत दूसरों को सुख-समृद्धि प्रदान करती है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने व देश की प्रगति के लाने के लिए भारतीय कृषक की प्रगति नितान्त आवश्यक है।

9. राष्ट्रीय ध्वज की कहानी
सकेत : भूमिका, राष्ट्रीय ध्वज के लिए अनेक प्रयास, भारतीय नेताओं के प्रयास, कांग्रेस की कार्य-समिति द्वारा निर्मित ध्वज, वर्तमान ध्वज का स्वरूप, उपसंहार।
राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने के लिए हम मूर्तियाँ, मंदिर, मस्ज़िद, धर्म-ग्रंथ, राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्र-गान एवं संविधान आदि प्रतीक बना लेते हैं। इन सबके प्रति आदर भाव रखने का अभिप्राय देश-प्रेम के भावों को पुष्ट एवं विकसित करना है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व हमारे देश का कोई झंडा नहीं था। भारत में तब ‘यूनियन जैक’ का ही बोलबाला था। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर इसे ही प्रमुखता मिलती थी। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भी सन् 1920 तक ‘यूनियन जैक’ की ही प्रतिष्ठा थी।
राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रयास सन् 1905 के आस-पास हुआ। इस प्रयत्न से देश के नवयुवकों में एक नवीन जागृति का संचार हुआ। कुछ देश-प्रेमी युवक उन दिनों विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने वहाँ देखा कि विदेशी जनसामान्य अपने देश के झंडे का कितना सम्मान करता है। उसकी रक्षा के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाता है और जब विदेशी भारतीय युवकों से उनके राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कोई प्रश्न करते तो उन्हें शर्म से सिर झुका लेना पड़ता था। अतः इस अपमानजनक परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए इन युवकों ने सोचा कि एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जाए, जिसे वे अपना कह सकें तथा जिसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करके गौरव का अनुभव कर सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के प्रथम झंडे के निर्माण की प्रथम भूमिका विदेशों में बनी।
विदेश में रह रहे भारतीय नवयुवकों ने उस समय जो झंडा तैयार किया, वह हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज से मिलताजुलता था। उसमें नीचे की पट्टी हरी, बीच की सफेद और ऊपर की केसरिया थी, जिसे सूर्य, अर्द्ध चंद्र तथा तारे से सजाया गया था और बीच की सफेद पट्टी पर ‘वंदे मातरम्’ लिखा गया था। केसरिया पट्टी पर आठ कमल बने थे जो भारत के तत्कालीन आठ प्रांतों के सूचक थे, लेकिन भारतीय राजनेताओं ने इस झंडे को स्वीकार नहीं किया और उन युवकों का प्रयास असफल रहा।
सन 1917 में डॉ० ऐनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक ने एक झंडे का निर्माण किया। इस झंडे पर बड़ी-बड़ी पट्टियाँ तथा तारे थे और एक किनारे पर यूनियन जैक था। परंतु इस झंडे को भी अस्वीकार कर दिया गया। सन् 1921 में लाला हंसराज, महात्मा गांधी के पास एक झंडा लेकर आए, जिसमें लाल और हरे रंग की दो पट्टियाँ थीं, जो भारत के दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम एकता की द्योतक थीं। तब महात्मा गांधी ने अन्य धर्मों के सूचक सफेद रंग तथा चरखे के चिह को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। तब एक ऐसा ध्वज बनाया गया, जिसमें नीचे की पट्टी लाल, बीच की हरी तथा ऊपर की सफेद थी और इन पर चरखे का चिह्न भी था। हर राष्ट्रीय आयोजन में इस झंडे को गौरवपूर्ण स्थान मिलने लगा।
इस राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंग संप्रदाय सूचक थे, इसलिए आगे चलकर उनके संबंध में अनेक मतभेद हुए। तब कांग्रेस कार्य समिति ने एक सर्वमान्य झंडा तैयार किया, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर केसरिया, सफेद और हरा रंग थे। सफेद पट्टी पर नीले रंग का चरखा भी बनाया गया था। केसरिया रंग धैर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य और शांति का तथा हरा विश्वास, प्रताप, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना गया। 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस तिरंगे को देश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बहुमत से स्वीकार कर लिया गया।
22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के.जिस रूप को भारत की विधानसभा में स्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रमुख परिवर्तन था। ध्वज के मध्य में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र सम्मिलित किया गया तथा उसे भारत का राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। पं० जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में स्वतंत्र भारत के ध्वज को प्रस्तुत करते समय घोषणा की कि हमने एक ऐसे ध्वज को रूप देने का प्रयास किया है, जो देखने में सुंदर हो, जो संयुक्त रूप में तथा अलग-अलग रूपों में भी हज़ारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति या देश की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके।
इस प्रकार तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया। यह हमारे राष्ट्र का आदर्श चिह्न है और भारत का गौरव है। देश के सभी महत्त्वपूर्ण आयोजनों मे इसे प्रमुखता तथा प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा इसकी रक्षा का प्रण करते हैं। 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजपथ पर ध्वज फहराते हैं और सलामी लेते हैं। पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी भवनों पर फहराया जाता था, परंतु अब देश का हर नागरिक इसे हर भवन पर फहरा सकता है। हमारा तिरंगा झंडा हम सब भारतवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक है तथा हम सबका यह कर्त्तव्य है कि हम अपना सर्वस्व बलिदान कर इसकी रक्षा करें। इसे देखते ही प्रत्येक भारतवासी के मुख से बरबस निकल पड़ता है-
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊँचा रहे हमारा।

10. भारत और परमाणु शक्ति
संकेत : भूमिका, परमाणु की प्राचीन अवधारणा, प्राथमिक परीक्षण, परमाणु परीक्षण के दुष्परिणाम, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए आणविक शक्ति का प्रयोग, भारत में परमाणु विस्फोट, उपसंहार।
प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष हैं-अनुकूल और प्रतिकूल। किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु का उचित प्रयोग मानव और समाज के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वही हमारे लिए घातक बन जाता है। परमाणु शक्ति की स्थिति भी लगभग ऐसी है। आज विज्ञान का युग है और इस युग में परमाणु शक्ति की सर्वाधिक चर्चा हो रही है। परमाणु शक्ति जहाँ एक ओर मानव के लिए वरदान है, वहाँ दूसरी ओर अभिशाप भी है। जहाँ इसका प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए किया जाता है, वहीं इसे मानव के विनाश के लिए भी प्रयुक्त किया जा रहा है।
यद्यपि आज ‘परमाणु’ शब्द सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसकी अवधारणा आज से 3000 वर्ष पूर्व थी। कुछ आलोचकों के मतानुसार परमाणु की सर्वप्रथम धारणा भारत, चीन और यूनान में थी। संभवतः भारतीय मनीषियों को इसके बारे में समुचित ज्ञान रहा होगा लेकिन धीरे-धीरे यह धारणा लुप्त हो गई। विशेषकर, मध्यकाल में भोग-विलास की प्रबलता थी। भारत जैसा समृद्ध राष्ट्र परतंत्रता का शिकार बन गया और यहाँ का ज्ञान अंधकार के गर्त में छिप गया। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व एक अंग्रेज़ विद्वान डाल्टन ने परमाणु की धारणा को पुनर्जीवित किया। तत्पश्चात, आइंस्टीन ने ऊर्जा शक्ति का आविष्कार करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
परमाणु का प्रथम विस्फोट रदरफोर्ड नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने किया। जैसे-जैसे विज्ञान विकास करता चला गया, वैसे-वैसे परमाणु का महत्त्व भी बढ़ता गया। सन 1939 में यूरेनियम के न्यूट्रॉन प्रेरित विस्फोट की खोज से परमाणु शक्ति के भंडार खुल गए। धीरे-धीरे मानव जाति परमाणु शक्ति के रहस्य को समझने लगी। जर्मन वैज्ञानिकों की सहायता से अमेरिका ने इस दिशा में असंख्य प्रयोग किए। यहाँ तक कि परमाणु बम का आविष्कार भी कर लिया गया। विश्वविख्यात भौतिक विज्ञानवेत्ता डॉ० रॉबर्ट ओपेनहाइम को ही परमाणु बम का जनक माना जाता है। 13 जुलाई, 1945 को एलामोगेडरो रेगिस्तान में प्रथम बम का परीक्षण संपन्न हुआ।
इस विस्फोट से कुकुरमुत्ते के आकार का एक विशालकाय बादल उठा जो लगभग 40,000 फुट ऊँचा था। 9 मील तक झुलसाने वाली गर्मी थी और एक मील के घेरे के सभी प्राणी मृत्यु के शिकार बन गए थे परंतु 6 अगस्त, 1945 का दिवस मानवता के लिए सर्वाधिक करुणा का दिवस था। इस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो नगरों पर अणु बमों की वर्षा की। तीन लाख जनसंख्या का नगर क्षण भर में नष्ट-भ्रष्ट हो गया।
परमाणु के इस भयंकर विस्फोट से संसार भयभीत हो गया। कई देशों में इस भय ने उलटा ही प्रभाव किया। उन्होंने भी परमाणु बमों का आविष्कार किया। रूस, इंग्लैंड, चीन इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त, कतिपय अन्य देश भी इस ओर कार्यरत हैं। भारत भी परमाणु बम बनाने में सक्षमता प्राप्त कर चुका है किंतु अहिंसावादी देश होने के कारण वह इसका प्रयोग केवल शांति के क्षेत्र में ही करना चाहता है। परमाणु शक्ति का जहाँ विध्वंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ इसका मानव के कल्याण एवं भलाई के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
परमाणु शक्ति के प्रयोग से रेगिस्तान तथा बंजर धरती को उपजाऊ बनाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। रूस में परमाणु शक्ति के प्रयोग से बड़े-बड़े पर्वतों को काटकर सड़कें बनाई गई हैं। अणु शक्ति का प्रयोग कोयला, तेल तथा जल के स्थान पर होने लगा है। कुछ वर्ष पूर्व केवल अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड तथा चीन ही आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र थे। आज आणविक अस्त्रों का उत्पादन करना प्रत्येक राष्ट्र के सम्मान का सूचक बन गया है।
जनमत की इच्छाओं का समुचित सम्मान करते हुए भारत सरकार ने 1948 में अणु शक्ति आयोग की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य था-अणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग। डॉ० होमी जहाँगीर भाभा को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉ० भाभा की अध्यक्षता में प्रथम परमाणु प्रतिकार (रिऐक्टर) की ट्रांबे में (मुंबई के समीप) स्थापना की गई। परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए तारापुर में बिजलीघर का निर्माण किया गया।
24 जनवरी, 1966 को भारतीय आणविक वैज्ञानिक डॉ० होमी जहाँगीर भाभा वायुयान दुर्घटना में अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, लेकिन उनकी परंपरा को जीवित रखते हुए भारतीय विद्वानों ने 18 मई, 1974 को प्रातः 8 बजकर 5 मिनट पर देश के पश्चिमी भाग, राजस्थान के बाड़मेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर अपना प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट किया। इसी प्रकार, 11 मई और 13 मई, 1998 को पोखरण नामक स्थान पर दूसरा भूमिगत परमाणु विस्फोट किया गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के साथ छठा अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया।
अंत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे बढ़े हैं। एक ओर चीन के पास विशाल सेना और आणविक हथियारों का भंडार है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का भारत के साथ अघोषित युद्ध तो चल ही रहा है। अमेरिका आदि अन्य परमाणु संपन्न देशों की प्रतिक्रिया हम भली प्रकार से जानते हैं। यदि वे भारतीय दृष्टि के प्रति संवेदनशील होते तो शायद भारत को परीक्षण की आवश्यकता ही न पड़ती। भारत को अपने हितों को देखना है। यद्यपि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव के कल्याणार्थ करना चाहता है तथापि देश की रक्षा के लिए परमाणु हथियार नितांत आवश्यक हैं। इसीलिए भारत ने यह आणविक विस्फोट किया है।

11. पंचायती राज
पंचायती राज का मुख्य भाव है-जनता द्वारा चुनी गई वह संस्था जो गाँव की विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रबन्ध करती है। गाँव के विकास के साधन जनता सहमति से जुटाती है। भारतवर्ष में पंचायत की व्यवस्था बहुत ही प्राचीनकाल से चली आ रही है। वहाँ की जनता का पंचायत में पूर्ण विश्वास रहा है। पंचायती राज अर्थात् पंचायतों का गठन उन पाँच व्यक्तियों पर आधारित हुआ करता था जिनका चुनाव गाँव-बिरादरी के सामने गाँव के लोगों द्वारा ही होता था। यही पाँच व्यक्ति अपना एक मुखिया चुन लेते थे, जिसे सरपंच कहा जाता था। बाकी सभी पंच या सदस्य पंचायत कहलाते थे। दूर-दराज के देहातों एवं गाँवों में रहने वाले लोगों की अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए राजधानी व शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। गाँव की समस्याएँ गाँव में ही सुलझा ली जाती थीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इन पंचायतों व पंचायती राज-व्यवस्था का गठन किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। गाँव-देहात की कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर ये पंचायतें उनका निर्णय निष्पक्ष रूप से करती थीं। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद पंचों की सहमति से सरपंच जो भी निर्णय करता था, उसे पंच परमेश्वर का फैसला मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। ऐसी पंचायती राज परम्परा प्राचीनकाल से ही चली आ रही थी।
भारत के लिए यह व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं थी। यह एक प्राचीन बुनियादी व्यवस्था है। पहले बड़े-बड़े सम्राट भी इन्हीं पंचायतों के माध्यम से अपनी न्याय-व्यवस्था को जन-जन तक पहुँचाया करते थे। आज भी शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाया गया है। पंचायत के ऊपर कई गाँवों की खण्ड पंचायत होती थी। यदि स्थानीय पंचायत कोई निर्णय नहीं कर पाती या फिर उसका निर्णय किसी पक्ष को स्वीकार नहीं होता था तो मामला खण्ड पंचायत के सामने लाया जाता था। खण्ड पंचायत के ऊपर होती थी पूरे जिले की ‘सर्वग्राम पंचायत’।
भारत में अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था लागू होने पर इन पंचायतों की उपेक्षा कर दी गई और अपनी न्याय प्रणाली को थोंप दिया गया था। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनः संगठित किया। फलतः भारतीय संविधान की रचना करते समय इस विषय को नीति-निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत रखा गया। किन्तु यह व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं हो सकी। देखा यह भी गया है कि कुछ वर्षों से यह फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के विकास के लिए कुछ कार्य पंचायतों के सुपुर्द किए गए हैं। इस बीच पंचायतों के चुनाव भी हुए हैं। सन् 1993 में वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पंचायती राज पर वाद-विवाद के बाद इसका संशोधित विधेयक बहुमत से संसद में पास कर दिया गया है।
यह अत्यन्त सुखद विषय है कि भारतवर्ष में फिर से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है। महिलाएँ भी मैम्बर पंचायत एवं सरपंच चुनी जाती हैं। पूरे देश में इससे महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई है। आज ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रम इन पंचायतों के माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं। निश्चय ही गाँवों में पंचायतों के पुनर्गठन से गाँवों के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। देश में लोकतंत्र की मज़बूती के लिए पंचायतों का सुचारु रूप से चलना और सुदृढ़ होना नितान्त आवश्यक है। किन्तु थोड़ा अफसोस भी है कि जहाँ प्राचीनकाल में पंचायती राज व पंचायत के गठन में आपसी सहमति ही प्रधान थी आज पंचायत के चुनाव भी राजनीति के अखाड़े बन गए हैं और आपसी सहमति की अपेक्षा वोट की शक्ति बन गई है। इससे गाँव के आपसी सहयोग व प्रेम की भावना को ठेस पहुंची है।
12. ‘परहित सरस धर्म नहिं भाई’
अथवा
परोपकार
सकेत : भूमिका, परोपकार का अर्थ, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म, परोपकार से अलौकिक आनंद, परोपकार का वास्तविक स्वरूप, परोपकार जीवन का आदर्श, उपसंहार।
कविवर रहीम लिखते हैं-
‘तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान।
कहि रहीम परकाज हित, संपत्ति संचहि सुजान।।
भगवान ने प्रकृति की रचना इस प्रकार की है कि उसके मूल में परोपकार ही काम कर रहा है। उसके कण-कण में परोपकार का गुण समाया है। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती, बादल जलरूपी अमृत हमें देते हैं, सूर्य रोशनी देकर चला जाता है। इस प्रकार सारी प्रकृति परहित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करती रहती है।
‘परोपकार’ दो शब्दों ‘पर’ + ‘उपकार’ के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दूसरों का भला। जब मनुष्य ‘स्व’ की संकुचित सीमा से बाहर निकलकर ‘पर’ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है, वही परोपकार कहलाता है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने भी कहा है-‘मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे’। परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है अन्यथा आहार, निद्रा आदि तो मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। परहित के कारण ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियाँ तक दान में दे दी थीं। महाराज शिवि ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का माँस तक दे दिया था तथा अनेक महान् संतों ने लोक-कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था।
परोपकार मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य के पास विकसित मस्तिष्क तथा संवेदनशील हृदय होता है। दूसरों के दुःख से दुखी होकर उसके मन में उनके प्रति सहानुभूति पैदा होती है और वह उनके दुःख को दूर करने का प्रयत्न करता है तथा परोपकारी कहलाता है। परोपकार का सीधा संबंध दया, करुणा और संवेदना से है। सच्चा परोपकारी करुणा से पिघलकर हर दुखी प्राणी की सहायता करता है। ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ उक्ति भी परोपकार की ओर संकेत करती है।
परोपकार में स्वार्थ की भावना नहीं रहती। परोपकार करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। भाईचारे तथा विश्व-बंधुत्व की भावना बढ़ती है। सुख की जो अनुभूति किसी व्यक्ति का संकट दूर करने में, भूखे को रोटी देने में, नंगे को कपड़ा देने में, बेसहारा को सहारा देने में होती है, वह किसी अन्य कार्य करने से नहीं मिलती। परोपकार से अलौकिक आनंद मिलता है।
आज का मानव भौतिक सुखों की ओर बढ़ता जा रहा है। इन भौतिक सुखों के आकर्षण ने मनुष्य को बुराई-भलाई से दूर कर दिया है। अब वह केवल स्वार्थ-सिद्धि के लिए कार्य करता है। आज मनुष्य थोड़ा लगाने तथा अधिक पाने की इच्छा करने लगा है। जीवन के हर क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है। जिस कार्य से स्वहित होता है, वही किया जाता है, उससे चाहे औरों को कितना ही नुकसान उठाना पड़े। पहले छल-कपट, धोखे, बेईमानी से धन कमाया जाता है और फिर धार्मिक स्थलों अथवा गरीबों में थोड़ा धन इसलिए बाँट दिया जाता है कि समाज में उनका यश हो जाए। इसे परोपकार नहीं कह सकते।
महात्मा ईसा ने परोपकार के विषय में कहा था कि दाहिने हाथ से किए गए उपकार का पता बाएँ हाथ को नहीं लगना चाहिए। पहले लोग गुप्त दान दिया करते थे। अपनी मेहनत की कमाई से किया गया दान ही वास्तविक परोपकार होता है। न केवल मनुष्य अपितु राष्ट्र भी स्वार्थ केंद्रित हो गए हैं, इसीलिए चारों ओर युद्ध का भय बना रहता है। चारों ओर अहम् और स्वार्थ का राज्य है। प्रकृति द्वारा दिए गए निःस्वार्थ समर्पण के संदेश से भी मनुष्य ने कुछ नहीं सीखा। हजारों-लाखों लोगों में से विरले इंसान ही ऐसे होते हैं, जो पर-हित के लिए सोचते हैं।
परोपकारी व्यक्ति का जीवन आदर्श माना जाता है। वह सदा प्रसन्न तथा पवित्र रहता है। उसे कभी आत्मग्लानि नहीं होती, वह सदा शांत मन रहता है। उसे समाज में यश और सम्मान मिलता है। वर्तमान युग के महान् नेताओं महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक आदि को लोक-कल्याण करने के लिए सम्मान तथा यश मिला। ये सब पूजा के योग्य बन गए। परहित के कारण गांधी ने गोली खाई, ईसा सूली पर चढ़े, सुकरात ने जहर पिया। किसी भी समाज तथा देश की उन्नति के लिए परोपकार सबसे बड़ा साधन है। हर व्यक्ति का धर्म है कि वह परोपकारी बने। कवि रहीम ने परोपकार की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है
“रहिमन यों सुख होत है उपकारी के अंग।
बाटन वारे को लगे ज्यों मेंहदी के रंग।’
अर्थात् जिस प्रकार मेंहदी लगाने वाले अंगों पर भी मेंहदी का रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार परोपकार करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी सुख की प्राप्ति होती है।

13. आदर्श खिलाड़ी के गुण
मानव-जीवन एक यात्रा के समान है। यदि यात्री को ज्ञात हो कि उसे कहाँ जाना है तो वह उसी दिशा में अग्रसर होता है। यदि उसे अपने लक्ष्य का बोध न हो तो उसकी यात्रा ही निरर्थक हो जाती है। इसी प्रकार यदि एक युवक को पता हो कि उसे क्या करना है तो वह उसी दिशा में प्रयास करना आरम्भ कर देता है। उसे सफलता भी प्राप्त होती है। यही बात एक आदर्श खिलाड़ी पर भी लागू होती है। जब एक खिलाड़ी अपने जीवन का लक्ष्य किसी खेल को खेलना बना लेता है तो उसे उसी दिशा में आगे बढ़ना होता है। आज के युग में कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें शोहरत के साथ-साथ धन की प्राप्ति भी अत्यधिक है। खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी पैसे कमाने को अहमियत देते हैं। किन्तु जो खिलाड़ी पूरे प्राणपन से अपने खेल के प्रति समर्पित होता है और देश की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर खेलता है उसे ही आदर्श खिलाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है।
आदर्श खिलाड़ी का पहला गुण खेल के प्रति समर्पण की भावना होती है। खेल भले ही कोई भी हो सकता है किन्तु एक आदर्श खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान और प्राणपन खेल के प्रति रखता है। तभी वह उस खेल में जीत हासिल कर सकता है और प्रसिद्धि की बुलंदियों को छू सकता है। अधूरे मन से खेलने वाला खिलाड़ी न तो खेल में विजयी हो सकता है और न ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः खेल के प्रति समर्पण की भावना आदर्श खिलाड़ी का प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण गुण है।
यद्यपि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का पालन करना अति आवश्यक है। अनुशासन से मानव-जीवन समृद्ध होता है। इसी प्रकार अनुशासनप्रियता खिलाड़ी का अहम् गुण होता है। अनुशासन में रहने का तात्पर्य है कि खेल के नियमों का पालन करना। यदि कोई खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन करता हुआ उस खेल को खेलता है तो उसे निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। विजय न भी प्राप्त हो किन्तु उसे अनुशासनहीन नहीं कहा जा सकता। विजय तो कभी-न-कभी उसे मिलेगी ही। यहाँ हम क्रिकेट के सम्राट सचिन तेंदुलकर को उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं। उन्होंने अपने खेल के जीवन में कभी भी खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। आज उन्हें उनके सर्वाधिक रन बनाने व सफल खिलाड़ी के साथ-साथ अनुशासन प्रिय खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
कहावत भी है कि “करत-करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान।” इस कहावत का भाव है कि किसी भी कार्य में निरन्तर अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकता है। अपने खेल का निरन्तर अभ्यास करना आदर्श खिलाड़ी का एक महत्त्वपूर्ण गुण है। बिना अभ्यास के किसी भी कार्य में कुशलता व निपुणता हासिल नहीं हो सकती। यही बात खेल और खिलाड़ी पर भी लागू होती है। इतिहास गवाह है कि अभ्यास से ही साधारण स्तर के खिलाड़ी भी खेल में विजयी होते हैं। महाभारतकालीन एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने है। उसने अभ्यास के बल पर ही तीर चलाने में इतनी निपुणता प्राप्त की थी कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए थे। अतः स्पष्ट है कि निरन्तर अभ्यास करना एक आदर्श एवं सच्चे खिलाड़ी का प्रमुख गुण है।
समभावता का अभिप्राय है कि हार व जीत को समान भाव से ग्रहण करना। एक आदर्श खिलाड़ी हार जाने पर कभी निराश नहीं होता, अपितु हार से सबक लेकर भविष्य में विजय प्राप्त करने का निश्चय लेकर पुनः खेल के मैदान में उतरता है। एक आदर्श खिलाड़ी विजयी होने पर कभी घमण्डी व अहंकारी नहीं बनता और न ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। वह विजयी होने पर शांत व सरल स्वभाव युक्त बना रहता है। भारतीय क्रिकेट टीम के जाने-माने खिलाड़ी व पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी इसके उदाहरण हैं। वे विजयी होने पर भी पूर्ववत शांत एवं सहज बने रहते हैं।
कोई भी महान खिलाड़ी सदैव दूसरे खिलाड़ियों का सम्मान करता है। टीम के दूसरे खिलाड़ियों का सम्मान करने से आदर्श खिलाड़ी की उदारता का पता चलता है। दूसरे खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना ही खिलाड़ियों का सम्मान करना है। दूसरे खिलाड़ियों के खेल की सराहना करना भी उनका सम्मान करना है। दूसरे का सम्मान करना अर्थात् स्वयं भी सम्मानित होना है। इस गुण के आधार पर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के मन में सम्मान का एक विशेष स्थान बना लेता है।
एक आदर्श खिलाड़ी सदा धैर्यशील बना रहता है। वह खेल में कभी अपना धैर्य नहीं खोता। स्वयं धैर्यशील रहकर अपने अन्य खिलाड़ी साथियों को धीरज बंधाता है। कभी-कभी तो धैर्यशील खिलाड़ी को देखकर पूरी-की-पूरी टीम उत्साह एवं उमंग में भरकर खेलती है। ऐसे में खेल में विजयी होना आसान बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि धैर्यशीलता आदर्श खिलाड़ी का महत्त्वपूर्ण गुण है।
टीम की भावना अर्थात् सबके साथ मिलकर खेलने की भावना आदर्श खिलाड़ी का अन्य महत्त्वपूर्ण गुण है। एक आदर्श खिलाड़ी सदा व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने की भावना की अपेक्षा पूरी टीम को विजयी बनाने की भावना मन में रखकर खेल के मैदान में उतरता है। वह भली-भांति जानता है कि यदि टीम खेलं में हारती है तो उसका व्यक्तिगत स्कोर या रिकॉर्ड किसी काम का नहीं। टीम के विजयी होने से किसी देश का सम्मान अधिक बढ़ता है, न कि एक खिलाड़ी के अच्छे खेलने से। इसलिए एक आदर्श खिलाड़ी टीम भावना से भरपूर होता है और इसी भावना को लेकर खेलता है।
एक आदर्श खिलाड़ी सदैव सहनशील होता है। दूसरे उसे क्या कहते हैं या उसे कुछ गलत कहकर खेल से भटकाने का प्रयास करते हैं तो उस समय वह उनके कथनों की ओर या तो ध्यान नहीं देता या उन्हें सहज ही सहन करते हुए अपने खेल पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करके खेलता है। ऐसे सहनशील खिलाड़ी सदा ही सम्मान के पात्र बने रहते हैं। विरोधी दल (टीम) के खिलाड़ी भी उसका मान-सम्मान करते हैं।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आदर्श खिलाड़ी के लिए उसका प्रमुख लक्ष्य खेल में विजयी होना होता है। वह उपर्युक्त सभी गुणों को जीवन में धारण करते हुए एक आदर्श स्थापित करता है। वह अपने खेल के प्रति पूर्णतः ईमानदार बना रहता है। वह सदैव टीम की विजय को महत्त्व देता है और इससे भी बढ़कर अपने देश व राष्ट्र के सम्मान को अपने खेल के माध्यम से बढ़ाता है।

14. परिश्रम और भाग्य
अथवा
परिश्रम का महत्व
संकेत : भूमिका, भाग्य का सहारा, परिश्रम की विजय, परिश्रम के लाभ, महापुरुषों के उदाहरण, उपसंहार।
मानव जीवन में परिश्रम का विशेष महत्त्व है। मानव तो क्या, प्रत्येक प्राणी के लिए परिश्रम का महत्त्व है। चींटी का छोटा-सा जीवन भी परिश्रम से पूर्ण है। मानव परिश्रम द्वारा अपने जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझा सकता है। यदि वह चाहे तो पर्वतों को काटकर सड़क निकाल सकता है, नदियों पर पुल बाँध सकता है, काँटेदार मार्गों को सुगम बना सकता है और समुद्रों की छाती को चीरकर आगे बढ़ सकता है। ऐसा कौन-सा कार्य है जो परिश्रम से न हो सके। नेपोलियन ने भी अपनी डायरी में लिखा था’असंभव’ जैसा कोई शब्द नहीं है। कर्मवीर तथा दृढ़-प्रतिज्ञ महापुरुषों के लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्य पर निर्भर रहकर श्रम को छोड़ देते हैं। वे भाग्य का सहारा लेते हैं परंतु भाग्य जीवन में आलस्य को जन्म देता है और यह आलस्य जीवन को अभिशापमय बना देता है। आलसी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। ऐसा व्यक्ति हर काम को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। हमारा देश इसी भाग्य पर निर्भर रहकर सदियों तक गुलामी को भोगता रहा। हमारे अंदर हीनता की भावना घर कर गई लेकिन जब हमने परिश्रम के महत्त्व को समझा तब हमने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई और पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ डाला। संस्कृत के कवि भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति।
दैवं निहत्य करु पौरुषमात्माशक्तया, यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः॥
अर्थात् उद्यमी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है। ‘ईश्वर देगा’ ऐसा कायर आदमी कहते हैं। दैव अर्थात् भाग्य को छोड़कर मनुष्य को यथाशक्ति पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि परिश्रम करने पर भी कार्य सिद्ध न हों तो सोचना चाहिए कि इसमें हमारी क्या कमी रह गई है।
केवल ईश्वर की इच्छा और भाग्य के सहारे पर चलना कायरता है। यह अकर्मण्यता है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। अंग्रेज़ी में भी कहावत है-“God helps those who help themselves” अर्थात् ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। कायर और आलसी व्यक्ति से तो ईश्वर भी घबराता है। कहा भी गया है-‘दैव-दैव आलसी पुकारा।
संस्कृत की ही उक्ति है-‘श्रमेव जयते’ अर्थात परिश्रम की ही विजय होती है। वस्तुतः मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह स्वयं ईश्वर का प्रतिरूप है। संस्कृत का एक श्लोक है-
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥
इसका अर्थ यह है कि उद्यम से ही मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुँह में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार से मनुष्य को भी कर्म द्वारा सफलता मिलती है। कर्म से मानव अपना भाग्य स्वयं बनाता है। एक कर्मशील मानव जीवन की सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है।
परिश्रम से मनुष्य का हृदय गंगाजल के समान पावन हो जाता है। परिश्रम से मन की सभी वासनाएँ और दूषित भावनाएँ बाहर निकल जाती हैं। परिश्रमी व्यक्ति के पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं होता। कहा भी गया है-“खाली मस्तिष्क शैतान का घर है।” यही नहीं, परिश्रम से आदमी का शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है। उसके शरीर को रोग नहीं सताते । परिश्रम से यश और धन दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो भाग्य के भरोसे न रहकर थोड़े-से धन से काम शुरू करते हैं और देखते-ही-देखते धनवान बन जाते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी यश मिलता है और मरने के उपरांत भी। वस्तुतः परिश्रम द्वारा ही मानव अपने को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को ऊँचा उठा सकता है। जिस राष्ट्र के नागरिक परिश्रमशील हैं, वह निश्चय ही उन्नति के शिखर को स्पर्श करता है लेकिन जिस राष्ट्र के नागरिक आलसी और भाग्यवादी हैं, वह शीघ्र ही गुलाम हो जाता है।
हमारे सामने ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण हैं जिन्होंने परिश्रम द्वारा अपना ही नहीं अपितु अपने राष्ट्र का नाम भी उज्ज्वल किया है। अब्राहिम लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था लेकिन निरंतर कर्म करते हुए वे झोंपड़ी से निकलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, नेता जी सुभाषचंद्र बोस आदि महापुरुष इस बात के साक्षी हैं कि परिश्रम से ही व्यक्ति महान बनता है।
यदि हम चाहते हैं कि अपने देश की, अपनी जाति की और अपनी स्वयं की उन्नति करें तो यह आवश्यक है कि हम भाग्य का सहारा छोड़कर परिश्रमी बनें। आज देश के युवाओं में जो बेरोज़गारी और आलस्य व्याप्त है, उसका भी एक ही इलाज हैपरिश्रम। संस्कृत में भी ठीक कहा गया है-
श्रमेण बिना न किमपि साध्यं।
15. काला धन
काले धन को अंग्रेज़ी में ‘ब्लैक मनी’ कहते हैं। अवैध तरीके अपनाकर कमाया गया धन काला धन कहलाता है। काला धन कमाने के अवैध तरीके हैं-आयकर की चोरी, अन्य प्रकार के कर का भुगतान न करना, चोर बाजारी में सामान बेचकर धन कमाना एवं राष्ट्र व मानवता विरोधी कार्यों द्वारा धन कमाना आदि। इस धन का लेखा-जोखा किसी भी सरकारी आँकड़ों में नहीं आता। काला धन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बन्धन होता है। काले धन को लोग विदेशों के बैंकों में जमा करते हैं, जहाँ आयकर का नियम लागू नहीं होता। सिंगापुर, मॉरीशस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि ऐसे ही देश हैं। भारतीयों का काला धन स्विट्ज़रलैण्ड के बैंकों में जमा होने की अनेक बार भर्त्सना हो चुकी है।
यह एक कटु सत्य है कि आज काले धन के बल पर काली अर्थव्यवस्था चल रही है। भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त होने वाला धन काली अर्थव्यवस्था में लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। काला धन काला बाज़ार भी तैयार करता है। इससे जन-साधारण के जीवन एवं अर्थ सम्बन्धी कष्ट व समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। काले धन के बल पर वस्तुओं का बाज़ार में अभाव दिखाकर उसकी बिक्री मनमाने दामों पर करके और भी अधिक काला धन बटोरा जाता है।
काले धन के कारण समाज में अनेक कुरीतियों, अपराधों आदि को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए काले धन से अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
ऐसा नहीं है कि सरकार काले धन की समस्या से अवगत नहीं है। देश के काले धन को सामने लाने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् समय-समय पर आयकर जाँच आयोग जैसे अनेक आयोगों का गठन किया गया। सरकार ने 1951 ई० में स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के तहत ₹ 70.2 करोड़ के काले धन का पता लगाया। इसी प्रकार 1968 ई० में सरकार की योजनाओं द्वारा पर्याप्त काले धन का पता लगाया गया। इसी प्रकार 1997 व 1998 में स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के तहत देश में ₹ 33000 करोड़ के काले धन का पता लगाया गया था।
हाल ही में विदेशों में काले धन से जुड़े खातों की जानकारी सार्वजनिक न करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को खरी-खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह केवल कर चोरी का मामला नहीं है, अपितु देश के साथ लूट का मामला है।
विदेशों के बैंकों में जमा काले धन के साथ-साथ अपने ही देश के लोगों के पास कितना धन, घर, ज़मीन, बैंक लॉकर्स या. तिजोरियों में बन्द पड़ा है, उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। यदि इस धन को देश की अर्थ-व्यवस्था में लगाया जाए तो इससे देश का विकास सहज हो सकता है। इससे काफी सीमा तक बेरोजगारी की समस्या भी कम हो सकती है।
काले धन की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों के साथ दोहरी कराधान संधि के साथ-साथ विमुद्रीकरण की नीति को भी व्यवहार में लाना लाभप्रद हो सकता है। जैसा कि मोदी सरकार ने 2016 ई० में नोटबंदी करके किया है। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है रुपए का पुनमुद्रण । जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। इसके अनुसार पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को प्रचलन में लाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जिसके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं करता। फलस्वरूप काला धन स्वतः नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष में यह प्रयोग काफी हद तक सफल रहा है। किन्तु काले धन के सौदागर भी कम चालाक नहीं निकले उन्होंने भी नए-नए हथकंडे अपनाए।
काले धन को बाहर लाने के लिए कर-व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए ईमानदार एवं कार्य-कुशल कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। आयकर विभाग द्वारा नियमित रूप से उद्योगपत्तियों व व्यापारियों तथा राजनेताओं के विभिन्न स्थानों पर जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। इससे काले धन को बाहर लाया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इससे देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा।

16. कुसंगति के दुष्परिणाम
संकेत : भूमिका, कुसंगति के दुष्परिणाम, सज्जन और दुर्जन का संग, कुसंगति से बचने के उपाय, सत्संगति के प्रकार, उपसंहार।
कुसंगति का शाब्दिक अर्थ है-बुरी संगति। अच्छे व्यक्तियों की संगति से बुद्धि की जड़ता दूर होती है, वाणी तथा आचरण में सच्चाई आती है, पापों का नाश होता है और चित्त निर्मल होता है लेकिन कुसंगति मनुष्य में बुराइयों को उत्पन्न करती है। यह मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाती है। जो कुछ भी सत्संगति के विपरीत है, वह कुसंगति सिखलाती है। एक कवि ने कहा भी है-
काजल की कोठरी में कैसे हू सयानो जाय,
एक लीक काजल की लागि हैं, पै लागि हैं।
यह कभी नहीं हो सकता कि परिस्थितियों का प्रभाव हम पर न पड़े। दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहने से सज्जन व्यक्ति का चित्त भी दूषित हो जाता है।
कुसंगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक कहावत है-अच्छाई चले एक कोस, बुराई चले दस कोस । अच्छी बातें सीखने में समय लगता है। जो जैसे व्यक्तियों के साथ बैठेगा, वह वैसा ही बन जाएगा। बुरे लोगों के साथ उठने-बैठने से अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति के चरित्र का पता लगाना हो तो पहले हम उसके साथियों से बातचीत करते हैं। उनके आचरण और व्यवहार से ही उस व्यक्ति के चरित्र का सही ज्ञान हो जाता है।
कुसंगति की अनेक हानियाँ हैं। दोष और गुण सभी संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जितना दुराचार, पापाचार, दुष्चरित्रता और दुर्व्यसन होते हैं, वे सभी कुसंगति के फलस्वरूप होते हैं। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को कुसंगति के प्रभाव से बिगड़ते हुए देखा जा सकता है। जो विद्यार्थी कभी कक्षा में प्रथम आते थे, वही नीच लोगों की संगति पाकर बरबाद हो जाते हैं। कुसंगति के कारण बड़े-बड़े घराने नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान-से-बुद्धिमान् व्यक्ति पर भी कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। कवि रहीम ने भी एक स्थल पर लिखा है-
बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम जिय सोच।
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यौ पड़ोस ॥
सज्जन और दुर्जन का संग हमेशा अनुचित है बल्कि यह विषमता को ही जन्म देता है। बुरा व्यक्ति तो बुराई छोड़ नहीं सकता, अच्छा व्यक्ति ज़रूर बुराई ग्रहण कर लेता है। अन्यत्र रहीम कवि लिखते हैं
कह रहीम कैसे निभै, बेर केर को संग।
वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग ॥
अर्थात् बेरी और केले की संगति कैसे निभ सकती है ? बेरी तो अपनी मस्ती में झूमती है लेकिन केले के पौधे के अंग कट जाते हैं। बेरी में काँटे होते हैं और केले के पौधे में कोमलता। अतः दुर्जन व्यक्ति का साथ सज्जन के लिए हानिकारक ही होता है।
हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें दुर्जनों की संगति छोड़कर सत्संगति करनी होगी। सत्संगति का अर्थ हैश्रेष्ठ पुरुषों की संगति। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान्, विद्वान् और गुणवान लोगों के संपर्क में आता है तो उसमें अच्छे गुणों का उदय होता है। उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति से मनुष्य की बुराइयाँ दूर होती हैं और मन पावन हो जाता है। कबीरदास ने भी लिखा है
कबीरा संगति साधु की, हरै और की व्याधि।
संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि ॥
सत्संगति दो प्रकार से हो सकती है। पहले तो आदमी श्रेष्ठ, सज्जन और गुणवान व्यक्तियों के साथ रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण करे। दूसरे प्रकार का सत्संग हमें श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त होता है। सत्संगति से मनुष्यों की ज्ञान-वृद्धि होती है। संस्कृत में भी कहा गया है- सत्संगति : कथय किं न करोति पुंसाम्। . रहीम ने पुनः एक स्थान पर कहा है.. . जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग ॥ अर्थात् यदि आदमी उत्तम स्वभाव का हो तो कुसंगति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यद्यपि चंदन के पेड़ के चारों ओर साँप लिपटे रहते हैं तथापि उसमें विष व्याप्त नहीं होता। महाकवि सूरदास ने भी कुसंगति से बचने की प्रेरणा देते हुए कहा है-
तज मन हरि-विमुखनि को संग।
जाकै संग कुबुधि उपजति है, परत भजन में भंग ॥
बुरा व्यक्ति विद्वान् होकर भी उसी प्रकार दुःखदायी है, जिस प्रकार मणिधारी साँप। मनुष्य बुरी संगति से ही बुरी आदतें सीखता है। विद्यार्थियों को तो बुरी संगति से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सिगरेट-बीड़ी, शराब, जुआ आदि बुरी आदतें व्यक्ति कुसंगति से ही सीखता है। अस्तु, कुसंगति से बचने में ही मनुष्य की भलाई है।

17. स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत
‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अभियान की शुरुआत सरकार द्वारा देश को स्वच्छता के प्रतीक रूप में पेश करना है। वस्तुतः स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गाँधी के द्वारा देखा गया था। इस विषय के सम्बन्ध में गाँधी जी ने कहा है-“स्वच्छता स्वतन्त्रता से ज्यादा जरूरी है।” इस कथन के पीछे का भाव है कि वे देश की गरीबी और गन्दगी से भली-भांति अवगत थे। उनके कथन का अर्थ है कि स्वच्छता में ही स्वस्थता की कल्पना की जा सकती है। स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी बेहतरी के सम्बन्ध में सोच सकता है। गाँधी जी ने अपने समय में इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया, किन्तु वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा था कि निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग हैं। किन्तु यह खेद का विषय है कि भारत की आज़ादी के इतने वर्षों तक भी भारत इन दोनों लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है। गाँवों में तो दशा और भी शोचनीय है। गाँधी जी के सपने को पूरा करने के लिए ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अभियान का शुभारम्भ 2 अक्तूबर, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया तथा इस मिशन को 2 अक्तूबर, 2019 तक पूरा करने का समय भी निश्चित किया।
‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अभियान राष्ट्रीय स्वच्छता की एक मुहिम है। इसके तहत भारत को सन् 2019 तक पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए गाँधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। यह आन्दोलन गाँधी जी के जन्मदिन (2 अक्तूबर, 2014) को शुरू हुआ और उनके जन्मदिन (2 अक्तूबर, 2019) को सम्पन्न होगा। भारत के शहरी विकास तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत इस अभियान को नगरों व गाँवों दोनों में लागू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सफाई व्यवस्था की समस्या का समाधान निकालना और साथ ही सभी को स्वच्छता की सुविधा के निर्माण द्वारा पूरे भारत में बेहतर मल प्रबन्धन करना है।
‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अभियान की आवश्यकता पर विचार करने से पता चलता है कि भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए भारत के लोगों में इसका एहसास होना अति आवश्यक है। यह सच्चे अर्थों में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए है। जो चारों ओर स्वच्छता लाने के लिए शुरू किया जा सकता है। यह जरूरी है कि हर घर में शौचालय बनाने के साथ-साथ खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। हाथ से साफ-सफाई की जाने वाली व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना नितान्त आवश्यक है।
नगर-निगम द्वारा कचरे का पुनर्चक्रण अथवा पुनः इस्तेमाल तथा वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबन्धन को लागू करना है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से ग्रामीण जनता स्वस्थता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी है। पूरे भारत में साफ-सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाना भी ‘स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत’ अभियान का महत्त्वपूर्ण भाग है। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को निरन्तर साफ-सफाई के प्रति जागरूक करना भी इस अभियान की आवश्यकता पर बल देता है। वास्तव में यह पूरा अभियान बापू के सपनों को पूरा करने की भावना के प्रति समर्पित है।
स्वच्छ भारत अभियान का मूल लक्ष्य शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबन्धन सहित लगभग 1.04 करोड़ घरों को, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम पाँच वर्षों के अन्दर अर्थात् 2019 तक पूरा करने की योजना है। इस अभियान का अन्य प्रमुख लक्ष्य खुले में शौच की प्रवृत्ति को जड़ से हटाना, अस्वास्थ्यकर शौचालय को पानी से बहाने वाले शौचालयों में परिवर्तन, खुले हाथों से साफ-सफाई की प्रवृत्ति को हटाना, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना और ठोस कचरा प्रबन्धन करना है।
‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अभियान में ग्रामीण स्वच्छ भारत का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत भारतीय गाँवों में स्वच्छता कार्यक्रम अमल में लाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए 1999 ई० में भारत सरकार द्वारा इससे पहले निर्मल भारत अभियान की स्थापना की गई थी। उसका लक्ष्य भी गाँवों को पूर्ण स्वच्छ बनाना था। किन्तु अब यह योजना ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ अभियान के अन्तर्गत पुनर्गठित की गई है। इसका लक्ष्य भी ग्रामीणों को खुले में शौच जोने से रोकना है। इसके लिए सरकार ने 11 करोड़, 11 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में ग्राम पंचायत, जिला परिषद् और पंचायत समितियों की भी सीधी भागीदारी होगी।
ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और उनके जीवन-स्तर को सुधारना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और द्रव्य कचरा प्रबन्धन पर खास तौर पर ध्यान देना तथा उन्नत पर्यावरणीय साफ-सफाई व्यवस्था का विकास करना, जो समुदायों द्वारा प्रबन्धनीय हो, इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है।
स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान भी ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत मिशन के तहत ही चलाया गया है। यह केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य विद्यालयों में स्वच्छता लाना है। इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक ही भाग लेते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों व नवोदय विद्यालय संगठनों द्वारा अनेक प्रकार के स्वच्छता क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं। यथा विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, महात्मा गाँधी की शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर चर्चा, स्कूलों में स्वच्छता क्रियाकलाप आदि। स्कूल क्षेत्र की सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी नाटक मंचन आदि अनेक गतिविधियाँ इन स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। आज जो विद्यार्थी हैं, वही कल नागरिक बनेंगे। इसलिए स्कूलों के साफ-सफाई सम्बन्धी क्रियाकलापों का अत्यधिक महत्त्व है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी भारतवासी और सरकार जब एक निश्चय से महात्मा गाँधी के ‘स्वच्छता ही सुख और स्वास्थ्य की नींव है’ के सपने को पूरा करने में जुट जाएँ तो इसे निश्चित व निर्धारित समय में हासिल किया जा सकता है। ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल भारतवासियों का लाभ होगा, अपितु विश्वस्तर पर भी भारत की छवि सुधरेगी। निश्चय ही स्वच्छता और स्वास्थ्य समाज और देश की जरूरत है। यदि स्वच्छता होगी तो स्वस्थता भी अवश्य बनी रहेगी। स्वच्छता में केवल स्वस्थता ही नहीं अपितु भगवान भी बसते हैं।

18. नर हो न निराश करो मन को
सकेत : भूमिका, छोटी-सी असफलता से निराश न होना, प्रकृति से प्रेरणा, निरंतर संघर्ष करना जीवन है, उपसंहार।
‘नर’ शब्द का सामान्य अर्थ पुरुष होता है। वस्तुतः नर और पुरुष एक शब्द के व्यंजन हैं। पुरुष का अर्थ भी नर है और नर का अर्थ पुरुष, किंतु ‘नर’ शब्द पर यदि गंभीरता या सूक्ष्मता से सोचा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि ‘नर’ शब्द के लाक्षणिक या व्यंजक प्रयोग से पुरुष की विशिष्टता को व्यक्त किया जाता है। पुरुष के पुरुषत्व तथा श्रेष्ठ वीरत्व के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ‘नर’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन अभिव्यंजित तथ्यों के प्रकाश में जब हम इस शीर्षक पंक्ति, ‘नर हो, न निराश करो मन को के अर्थ और भाव-विस्तार का विवेचन करते हैं तो मानव-जीवन के अनेक पक्ष स्वतः उजागर होने लगते हैं। मनुष्य के पौरुषत्व और पुरुषार्थ की महिमा जगमगा उठती है।
इस पंक्ति को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई हमें चुनौती भरे शब्दों में या ललकार भरी ध्वनि में कह रहा होवाह ! कैसे पुरुष हो तुम ! या अच्छे नर हो। तुम सांसारिक जीवन की छोटी-छोटी कठिनाइयों से ही घबरा उठते हो क्योंकि अभी तक तुमने जीवन की बाधाओं का सामना करना सीखा ही नहीं है। यों चिल्लाने लगे या घबराकर बोलने लगे कि जैसे आसमान टूट पड़ेगा अथवा जमीन फट जाएंगी। तुम पुरुष हो और वीरता तुम्हारे पास है। एक बार की असफलता से इतनी निराशा। उठो! और निराशा त्यागकर परिस्थितियों का डटकर सामना करो। हमें एक छोटी-सी चींटी से सबक सीखना चाहिए। जब वह चावल का दाना या कोई और वस्तु अपने मुँह में लेकर अपने बिल की ओर जा रही होती है तो उसका मार्ग रोककर देखो या उसके मुँह का दाना या भोजन छीन कर देखो, वह किस प्रकार छटपटाती है और बार-बार उस दाने को प्राप्त करने का प्रयास करती है। वह तब तक निरंतर संघर्ष करती रहेगी, जब तक दाना प्राप्त करके अपने बिल तक नहीं पहुँच जाती। एक ओर मनुष्य है जो थोड़ी-सी या छोटी-सी असफलता पर निराश होकर बैठ जाता है।
‘नर’ अर्थात् बुद्धि और बल से परिपूर्ण मनुष्य, प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाने वाला है। वह यदि जीवन में आने वाले संघर्ष या कठिनाइयों से मुँह फेरकर और निराश होकर बैठ जाए तो उसकी श्रेष्ठता के कोई मायने नहीं रह जाएँगे। उसे प्रकृति के हर छोटे-बड़े प्राणी से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि वह संघर्ष करना छोड़ देगा और निराश होकर बैठ जाएगा तो संसार में उसका विकास कैसे होगा ? हर प्रकार की उन्नति के मार्ग ही बंद हो जाएँगे। इसलिए मनुष्य को अपने नरत्व को सिद्ध करना होगा। उसे निराशा त्याग कर अपने हृदय में उत्साह और साहस भरकर जीवन-पथ को प्रशस्त करना होगा। यदि निराशा ही जीवन का तथ्य होती तो अब तक संसार में जो विकास हुआ है वह कभी संभव न हो पाता। नरता का पहला लक्षण ही आगे बढ़ना है, संघर्ष करते रहना है।
नदियों की बहती धारा की भाँति मनुष्य का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार धारा सागर में मिलकर ही विश्राम लेती है, उसी प्रकार नर को भी लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात ही दम लेना चाहिए। चट्टान भी धारा के मार्ग में आकर उसका रास्ता रोकने का प्रयास करती है। क्या कभी उस धारा को चट्टान रोक सकी ? क्योंकि अपने प्रबल प्रवाह से वह चट्टान को किनारे लगाकर अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। वह इस कार्य के लिए किसी से सहायता नहीं माँगा करती। झाड़-झंखाड़ों के रोके भी वह कभी नहीं रुकती। बहुत बड़ी चट्टीन के मार्ग में आ जाने पर भले ही धारा थोड़ी देर के लिए रुकी हुई-सी प्रतीत होती है, किंतु वह कुछ ही क्षणों में अपना दूसरा मार्ग खोज लेती है और फिर उसी प्रवाह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। नर (पुरुष) की भी जीवन-पद्धति या कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए। नर को भी समस्याओं के आने पर अपनी योजना बनाकर उनका सामना करना चाहिए और उन पर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तभी वह नर कहलाने योग्य बन सकता है। समस्याएँ सामने आने पर माथे पर हाथ रखकर तथा निराश होकर बैठ जाने से उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। वह तभी नर कहलाएगा जब वह समस्याओं पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगा। इसे ही सच्चे अर्थों में जीवन कहते हैं तथा यही नर के नरत्व को व्यक्त करता है।
नर होकर निराश बैठना, यह उसके लिए शोभनीय नहीं है। निराश होकर बैठ जाने और हिम्मत हार जाने वाले मनुष्य की स्थिति वैसी ही होगी जैसी मणि-विहीन सर्प की होती है। मणि ही सर्प की चमक का कारण होती है। उसी प्रकार हिम्मत एवं उत्साह ही मानव-जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले तत्त्व हैं। जब मनुष्य उनको त्यागकर बैठ जाता है तब वह ‘नर’ कहलाने का अधिकार भी खो बैठता है। ऐसा होना उसके लिए नरता से पतित होने, अपने आपको कहीं का भी नहीं रहने देने के समान होता है। इसलिए कहा गया है कि नर होकर मन को निराश न करो। मनुष्य को किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए।
निराशा जीवन में अंधकार भर देती है। इससे मनुष्य को कोई मार्ग नहीं सूझ सकता। इसके विपरीत, निराशा को त्यागकर आशावान और आस्थावान होकर जब मनुष्य समस्याओं से जूझता है तो उसका मार्ग स्वतः ही प्रकाशित हो उठता है और वह आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। संघर्ष और प्रयास में जो आनंद अनुभव होता है वह अमृत के समान होता है। संघर्ष को त्यागकर यदि हम निराशा का दामन पकड़ लेंगे तो उस अमृत के आनंद से भी हाथ धो बैठेंगे। अतः स्पष्ट है नर की नरता निराशा को त्यागकर संघर्ष करने में ही दिखाई देती है। इस पंक्ति का प्रमुख लक्ष्य ही निरंतर संघर्ष करना, गतिशील बने रहना, उत्साह और आनंद का संदेश देना है। इन्हीं से नर की नरता सार्थक होती हैं।

19. भारत की विदेश नीति
‘विदेश नीति’ से तात्पर्य है कि किसी भी देश को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का सामूहिक रूप होती है। किसी भी देश की या पूरे विश्व की स्थिति सदा एक समान नहीं रहती है। इसलिए बदलती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी भी देश की नीति में परिवर्तन होना भी आवश्यक होता है। इस संसार में कोई देश न तो किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी दुश्मन। विश्व इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं। भारतवर्ष की जो स्थिति 1947 में थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। इक्कीसवीं सदी में भारत को तेजी से उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जाता है। वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद, जलवायु
परिवर्तन, ऊर्जा संकट जैसी कठिनाइयों से निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबन्दी एवं सम्बन्धों में निरन्तर परिवर्तन होते रहे हैं। भारत को भी वर्तमान स्थिति के अनुकूल ही अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करने पड़े हैं अथवा विदेश नीति निश्चित की है।
स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने अपनी विदेश नीति तय की थी। उसका श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ-साथ विदेशमंत्री की भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने चीन आदि पड़ोसी देशों के साथ मित्रता की नीति अपनाई थी। विदेश नीति के तौर पर पंचशील की स्थापना भी की गई जिसका मूल उद्देश्य आपसी सहयोग और शांति को बढ़ावा देना था, किन्तु अक्तूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर उसका बड़ा भू-भाग हथिया लिया था। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। इसके पश्चात् सन् 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत के स्वतंत्र विदेश मंत्रालय की स्थापना की और विदेश मंत्री को नियुक्त किया। शास्त्री जी की नीतियों से भारत के दक्षिण-एशियाई देशों से सम्बन्ध बेहतर हुए। सन् 1965 में पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिमाकत की तो शास्त्री जी ने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े थे। सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत-पाकिस्तान समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत को पाकिस्तान के विजित क्षेत्र लौटाने पड़े। शास्त्री जी इस समझौते के पक्षधर नहीं थे। उनकी रहस्मय तरीके से ताशकंद में मृत्यु हो गई थी।
शास्त्री जी के पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गाँधी देश की प्रधानमंत्री बनीं। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की विदेश नीति में अनेक बदलाव किए। उन्होंने विदेश नीति को मजबूत बनाने के लिए गुप्तचर सेना को भी सुदृढ़ किया। उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पाकिस्तान की शक्ति क्षीण हुई थी। सन् 1974 में परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। इससे नाराज होकर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए। किन्तु 1971 में भारत ने सोवियत संघ से संधि कर ली थी। इससे न केवल आर्थिक अपितु सैन्य मदद भी भारत को मिली थी किन्तु सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हमला किया जाना, तब उसे भारत का समर्थन हासिल था। इस स्थिति को भारतीय विदेश नीति की एक विफलता के तौर पर देखा मया था।
श्रीमती इंदिरा गांधी के हार जाने पर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, किन्तु विदेश नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इन्दिरा जी की मृत्यु के पश्चात् श्री राजीव गाँधी ने अपने कार्यकाल में विदेश नीति को आधुनिक दशा एवं दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने के लिए चालीस देशों की यात्राएँ की थीं। श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में श्री राजीव गाँधी का हाथ था। इसके पश्चात् भारत की राजनीति में अस्थिरता का दौर आया। विदेश नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया।
1998 में अटलबिहारी वाजपेयी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने की विदेश नीति बनाई और उसमें वे सफल भी रहे। किन्तु पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ से भारत को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। 2001 में वाजपेयी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। वहाँ के राष्ट्रपति बिल-क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। यह काल भारतीय विदेश नीति की सफलता के काल के रूप में देखा जाता है।
सन् 2004 में डॉ० मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और वे दस वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे भारत की आर्थिक नीति को सुदृढ़ करने में सफल रहे। सन् 2008 में जब सारी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। 2006 में अमेरिका और भारत के बीच हुए सैन्य परमाणु समझौते ने भारत को अमेरिकी विदेश नीति में ऐसा स्थान दिला दिया जो किसी अन्य देश को हासिल नहीं है। इस समय अमेरिका का भारत के प्रति नरम रवैया अपनाना भारत की विदेश नीति की सफलता अवश्य मानी जाती है।
सन् 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें देश की जनता का पूर्ण बहुमत हासिल है। उन्होंने भारत की साख को विदेशों में बढ़ाने के लिए अनेक देशों से मित्रता का हाथ बढ़ाया। उनमें चीन, अमेरिका, रूस आदि प्रमुख हैं। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को सहायता देने की नीति को अपनाया है। मोदी जी भारत की छवि को अपनी विदेश नीति के माध्यम से सुधारने का सफल प्रयास कर रहे हैं। चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ भी उन्होंने अपनी कूटनीति से ही संबंधों में सुधार किया है। वर्तमान समय में भारत विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसलिए उसे अपनी विदेश नीति को भी समय व परिस्थितियों के अनुसार देश हित में निश्चित एवं निर्धारित करना होगा।
20. सदाचार का महत्त्व
अथवा
चरित्र का महत्त्व
संकेत : भूमिका, सदाचार एवं चरित्र का महत्त्व, स्वानुभव और चरित्र, विद्यार्थी जीवन और सच्चरित्रता, सदाचार के लाभ।
प्रत्येक मानव की यह इच्छा होती है कि समाज में उसका आदर-सम्मान हो। वस्तुतः आदर एवं सम्मान के बिना मनुष्य का अस्तित्व प्रकाश में नहीं आता। इसके लिए मानव अनेक साधनों का आश्रय लेता है। कोई धन के बल पर तो कोई सत्ता के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से कोई विद्या का आश्रय लेता है तो कोई अपनी शक्ति का। कोई समाज-सेवा द्वारा तो कोई चरित्र के बल पर नाम कमाना चाहता है। इन सब साधनों में से सच्चरित्रता ही जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्यों एवं समृद्धियों की आधारशिला है। यदि हम चरित्रवान हैं तो सभी हमारा आदर-सम्मान करते हैं। परंतु चरित्रहीन व्यक्ति समाज में निंदा और तिरस्कार का पात्र बनता है। वह समाज के लिए एक अभिशाप है। दुश्चरित्र व्यक्ति का जीवन अंधकारमय होता है, जबकि सच्चरित्र व्यक्ति ज्ञान एवं प्रकाश के उज्ज्वल वातावरण में वितरण करता है। प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त ने उचित ही कहा है-
“खलों का कहीं भी नहीं स्वर्ग है भलों के लिये तो यही स्वर्ग है।
सुनो स्वर्ग क्या है ? सदाचार है। मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।।”
अंग्रेजी की एक कहावत का भाव इस प्रकार है यदि मनुष्य का धन नष्ट हुआ तो उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, यदि उसका स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, परंतु यदि उसका चरित्र नष्ट हुआ तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। यह कहावत सच्चरित्रता के महत्त्व को दर्शाती है। सच्चरित्र बनने के लिए मनुष्य को सशिक्षा, सत्संगति और स्व + अनुभव की आवश्यकता होती है। परंतु यह जरूरी नहीं है। अनेक बार अशिक्षित व्यक्ति भी सत्संगति के कारण अच्छे चरित्र के देखे गए हैं। फिर भी बुद्धि का परिष्कार और विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। अच्छी शिक्षा के साथ-साथ सत्संगति भी अनिवार्य गुण है। संस्कृत में कहा भी गया है-
“संसर्ग जाः दोषगुणाः भवन्ति।”
अर्थात् दोष और गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। मानव जिस प्रकार के लोगों के साथ रहेगा, उनकी विचारधारा, व्यसन या आदतें उसे अवश्य प्रभावित करेंगी। सत्संगति नीच व्यक्ति को भी उत्तम बना देती है। कीड़ा भी फूलों की संगति पाकर सज्जनों के सिर की शोभा बनता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है-
“सठ सुधरहिं सत्संगति पाइ। पारस परस कुधातु सुहाई।।”
स्वानुभव भी मानव को चरित्रवान बनाने में काफी सहायक होता है। जब बच्चा एक बार आग को छूकर अँगुली जला बैठता है तो दुबारा अग्नि से सावधान रहता है। दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति जब दुष्ट कर्मों के परिणामों को जान लेता है तो वह दुबारा दुष्कर्म नहीं करता। व्यक्ति अपने अनुभव से यह जान लेता है कि अमुक काम करने से उसे यह फल भोगना पड़ा। यह बात बुरी है, उससे जीवन को हानि होती है अथवा झूठ बोलने से व्यक्ति को हानि होती है, लोगों में अपमान होता है तो वह झूठ बोलना छोड़ देता है। इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभव भी मनुष्य को सच्चरित्रता की ओर ले जाते हैं। सच्चरित्रता लाने के लिए हमें अपने पूर्वजों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए।
विद्यार्थी जीवन सच्चरित्रता के विकास के लिए सर्वाधिक उचित समय है। युवाकाल में विद्यार्थी का मन काफी कोमल होता है। उसे जैसा चाहो वैसा बनाया जा सकता है। विद्यार्थी जीवन उस साधनावस्था का समय है जिसमें बालक अपने जीवनोपयोगी अनंत गुणों का संचय करता है। वह इस काल में अपने मन और मस्तिष्क का परिष्कार कर सकता है। इसी काल में संयम और नियमों का पालन करना सीखता है। समय पर सोना, समय पर उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियमित रूप से अध्ययन करना, सज्जनों की संगति करना आदि विद्यार्थी को चरित्रवान बनाते हैं।
सच्चरित्रता से मानव अनेक प्रकार से लाभान्वित होता है। सच्चरित्रता किसी विशेष प्रवृत्ति की बोधक भी नहीं है। अनेक गुण जैसे-सत्य भाषण, उदारता, सहृदयता, विनम्रता, दयालुता, सुशीलता, सहानुभूतिपरता आदि समन्वित रूप से सच्चरित्रता कहलाते हैं। जो व्यक्ति चरित्रवान है, वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उसे समाज में आदर और सम्मान मिलता है, इस लोक में उसकी कीर्ति फैलती है तथा मरकर भी उसका नाम अमर हो जाता है। सच्चरित्र व्यक्ति की उच्च भावनाएँ तथा दृढ़ संकल्प हमेशा संसार में विचरण करते रहते हैं। सच्चरित्रता से व्यक्ति में शूरवीरता, धीरता, निर्भयता आदि गुण स्वतः आ जाते हैं, परंतु सदाचार एवं सच्चरित्रता के अभाव में मानव कदम-कदम पर ठोकरें खाता है, अपमानित होता है और पशु-तुल्य जीवन व्यतीत करता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम की सच्चरित्रता किसी से भी छिपी नहीं है। भारत के लाखों-करोड़ों नर-नारी उनके सच्चरित्र का अनुसरण करके अपने जीवन को पावन करते हैं। शिवाजी और महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएँ आज भी भारतीय जन-साधारण का मार्ग-दर्शन करती हैं। इसी प्रकार से आधुनिक काल में लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गाँधी, सुभाषचंद्र बोस आदि महान् विभूतियाँ भारतीयों के लिए अनुकरणीय हैं। इन महान् आत्माओं ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को छिन्न-भिन्न करने में अपने जीवन का बलिदान दिया। निश्चय ही सदाचार मानव को महान् बनाता है, एक साधारण व्यक्ति को भी युग-पुरुष बनाता है और उसे यश प्रदान करता है। संस्कृत में एक श्लोक है-
आचाराल्लभते आयुः आचारादीप्सिताः प्रजाः।
आचाराल्लभते ख्याति, आचाराल्लभते धनम् ।।
चरित्रवान् बनना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चरित्रता से मानव अपना कल्याण तो करता ही है, समाज का हित भी करता है। इससे वह सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। सच्चरित्रता से हम आज देश की असंख्य समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जिस राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र भ्रष्ट है, वह राष्ट्र कदापि विकास नहीं कर सकता। हमारे देश में फैली हुई गरीबी की जड़ भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता है। प्रमुख आलोचक एवं साहित्यकार डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “चरित्र बल हमारी प्रधान समस्या है। हमारे महान् नेता महात्मा गाँधी ने कूटनीतिक चातुर्य को बड़ा नहीं समझा, बुद्धि-विकास को बड़ा नहीं माना, चरित्र बल को ही महत्त्व दिया। आज हमें सबसे अधिक इसी बात को सोचना है। यह चरित्र-बल भी केवल एक व्यक्ति का नहीं, समूचे देश का होना चाहिए।”
अतः आज हमारा प्रमुख कर्त्तव्य यही है कि हम चरित्रवान बनें। विशेषकर, छात्र-छात्राओं को तो इस दिशा में भागीरथ प्रयत्न करने चाहिएँ, क्योंकि उन्हीं पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है।
21. मोबाइल का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग
विज्ञान के विकास से मानव को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। विज्ञान की उन्नति के कारण ही समाज में आशातीत परिवर्तन हुए हैं। इन चमत्कारिक परिवर्तनों में संचार के साधन में विकास भी एक चमत्कारयुक्त परिवर्तन है। संचार के साधनों में मोबाइल फोन एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यह एक त्वरित संप्रेषण अर्थात् शीघ्र ही सन्देश भेजने का प्रमुख साधन है। मोबाइल फोन का अर्थ है-चलता-फिरता फोन अर्थात जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज ही ले जाया जा सके। आरम्भ में मोबाइल फोन का प्रयोग बहुत कम लोग करते थे। किन्तु आज प्रत्येक छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित सब मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। आज मोबाइल केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गया है। आजकल मोबाइल फोन के बिना मानव-जीवन अधूरा-सा लगता है। निश्चय ही मोबाइल फोन ने मानव-जीवन को आसान बना दिया है। आज मोबाइल फोन की सहायता से विदेश में बैठा व्यक्ति अपने परिवार से न केवल बात करता है, अपितु साक्षात् उन्हें देख भी सकता है। यह मोबाइल का कितना बड़ा लाभ या सुविधा है। तीस वर्ष पूर्व इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
मोबाइल केवल मात्र फोन ही नहीं रह गया है अपितु इसमें इतनी अधिक अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं। इससे हम कैमरे का काम भी लेते हैं। केल्कुलेटर की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त इसमें रेडियो, गेम और टेपरिकॉडर आदि अनेक सुविधाएँ भी प्राप्त हैं। आज हमें आवाज के माध्यम से नहीं अपितु लिखित सन्देश भी भेज सकते हैं जिसे एस०एम०एस० कहते हैं। आज के युग को मोबाइल का युग कहना अनुचित नहीं है। इसके द्वारा हम एक-दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं। आज चिट्ठी अथवा पत्रों का कार्य मोबाइल फोन के माध्यम से करते हैं। धीरे-धीरे मोबाइल प्रतिष्ठा का विषय भी बनता जा रहा है। जिसके पास जितना महँगा मोबाइल उपलब्ध होगा उसका उतना ही स्टेटस आंका जाता है।
मोबाइल फोन का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है। विद्यार्थी जगत के लिए यद्यपि यह कहा जाता है कि उन्हें मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह कथन अर्द्ध सत्य है। विद्यार्थी हर विषय की जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में इन्टरनेट का प्रयोग भी होता है। व्यापारी लोग अपना हिसाब-किताब मोबाइल में रख सकते हैं। इसी प्रकार घरेलू महिलाओं के लिए मोबाइल जहाँ मनोरंजन का साधन है वहीं रसोई से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी उन्हें मोबाइल के माध्यम से प्राप्त होती है। मोबाइल फोन से समय की बचत होती है। आज बैंकों के लेन-देन भी इससे आसानी से हो जाते हैं। लेन-देन के लिए पंक्ति में खड़ा नहीं होना पड़ता। मोबाइल लाखों लोगों के रोजगार का साधन भी है।
आज हम मोबाइल के द्वारा मौसम की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें किसी अनजान स्थान पर जाना है तो उसके मानचित्र व उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी भी हमें मोबाइल से सहज ही प्राप्त हो सकती है। कहने का भाव है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज मोबाइल फोन उपयोगी सिद्ध हो रहा है।
उपर्युक्त वर्णन से अनुभव होता है कि मोबाइल के बिना तो आज का जीवन अधूरा है। किन्तु यदि गहराई से देखा व सोचा जाए तो पता चलता है कि जहाँ मोबाइल के इतने लाभ हैं अर्थात् मोबाइल ने मानव को इतनी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं, वहीं मानव-जीवन में अनेक असुविधाएँ भी पैदा करता है अर्थात् उससे अनेक हानियाँ भी होती हैं। आज मोबाइल कम्पनियाँ नित नई प्रतियोगिताओं के ऑफर दे रही हैं। इनकी चकाचौंध में फंसकर व्यक्ति अपना धन और समय दोनों बर्बाद कर रहा है। मोबाइल फोन मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अदृश्य किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती हैं। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मोबाइल फोन और भी खतरनाक सिद्ध हुआ है। इससे उनके मन-मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो उनकी आँखों के लिए हानिकारक है।
जैसा कि हमने पहले कहा है कि विद्यार्थियों के लिए मोबाइल लाभदायक है, किन्तु वहीं मोबाइल उस समय उनके लिए हानिकारक बन जाता है जब वे अनावश्यक चीजें व चित्र देखने व पढ़ाई व खेलकूद सब छोड़कर मोबाइल से चिपके रहते हैं। इससे न केवल युवा शक्ति प्रभावित होती है, अपितु देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य भी डावांडोल होने लगता है, क्योंकि युवाशक्ति ही देश का भविष्य होती है।
आज मोबाइल फोन अनेक सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन गया है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करने लगते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है जिससे वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
आज हर आयु वर्ग के लोगों के मन की एकाग्रता को भंग करने का कारण भी मोबाइल ही बन गया है। आप भले ही कितना जरूरी काम एकाग्रचित्त होकर कर रहे हों, किन्तु फोन या एस०एम०एस० आने से आपकी एकाग्रता टूट जाती है।
अपराध की दुनिया में भी मोबाइल का गलत प्रयोग किया जाता है। आतंकवादी व पत्थरबाज लोग भी मोबाइल का प्रयोग करके बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विज्ञान के ये आविष्कार हमारी सुख-सुविधाओं के लिए हैं किन्तु इनका अधिक दुरुपयोग किया जाता है। सही विकास तो वही माना जाता है जिससे मानव का समुचित विकास हो। निश्चय ही मोबाइल फोन के सदुपयोग द्वारा मानव-जीवन सुखी बनता है, किन्तु इससे उत्पन्न परेशानियों या हानियों के लिए मोबाइल नहीं अपितु हम स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी वस्तु का प्रयोग यदि एक सीमा एवं संयम में रहकर किया जाता है तो वह उपयोगी सिद्ध होता है। यदि हम इसका प्रयोग अनियन्त्रित होकर या बिना-सोचे समझे करेंगे तो उससे होने वाली हानियों के लिए हम ही उत्तरदायी होंगे। अतः मोबाइल का सही प्रयोग लाभदायक और दुरुपयोग हानिकारक है। दोनों के लिए उसका प्रयोगकर्ता ही जिम्मेदार है।

22. पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं
संकेत : उक्ति का अर्थ, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार, स्वतंत्र प्रकृति, पराधीनता के कारण विकास अवरुद्ध, भारत की पराधीनता, राष्ट्रोन्नति में स्वाधीनता का महत्त्व। महाकवि तुलसीदास ने कहा है-
पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं, सोच विचार देख मनमाही।
तुलसीदास जी की यह काव्य पंक्ति गहन अर्थ रखती है। इसका संदेश है कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, वह स्वजनों में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। पराधीनता वास्तव में अत्यंत कष्टदायक होती है।
हितोपदेश में कहा गया है-‘पराधीन को यदि जीवितं कहें तो मृत कौन है?” अर्थात् पराधीन व्यक्ति मृत के तुल्य है।
मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह किसी के अधीन या वश में रहने को तैयार नहीं होता। यदि कभी उसे पराधीन होना भी पड़े, तो वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी स्वाधीनता प्राप्त करना चाहता है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने कहा था, ‘स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी स्वाधीनता के महत्त्व तथा पराधीनता के कष्ट को जानते हैं। सोने के पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख तथा आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। सोने के पिंजरे में रहकर उसे षट्रस व्यंजन अच्छे नहीं लगते। वह तो पेड़ की डालियों पर बैठकर फल-फूल तथा दाना-तिनका खाने में आनंदित होता है।
प्रकृति का कण-कण स्वाधीन है। प्रकृति भी अपनी स्वाधीनता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहती। जब-जब मनुष्य ने अहंकार स्वरूप प्रकृति के स्वाधीन तथा उन्मुक्त स्वरूप के साथ छेड़खानी करने की चेष्टा की है, प्रकृति ने उसे सबक सिखाया। मनुष्य ने प्राकृतिक संतुलन तथा पर्यावरण को छेड़ने की कोशिश की तो परिणाम हुआ-प्रदूषण, भूस्खलन, बाटें, भू-क्षरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि। दो फूलों की तुलना कीजिए-एक उपवन में उन्मुक्त हँसी बिखेर रहा है तथा दूसरा फूलदान में लगा है। फूलदान में लगा पुष्प अपनी किस्मत पर रोता है, जबकि उपवन में लगा पुष्प आनंदित होता है। सर्कस में तरह-तरह के खेल दिखाने वाले पशु-पक्षी यदि बोल पाते तो रो-रोकर अपनी पराधीनता तथा कष्टों की कहानी सुनाते। वे बेचारे मूक प्राणी अपनी व्यथा को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते।
पराधीन व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। उसकी आत्मा तथा स्वाभिमान को पग-पग पर ठेस पहुंचती है। उसमें हीन भावना आ जाती है तथा उसका शौर्य, साहस, दृढ़ता तथा गर्व शनैः-शनैः शांत होने लगता . है। पराधीन व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। पराधीन व्यक्ति भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान बैठता है और कई बार तो वह इनसे भी वंचित रहता है। उसके सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसकी सृजनात्मक क्षमता भी धीरे-धीरे लुप्त होती चली जाती है।
भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। यह मानवता का महान सागर, गौरवशील देश लगभग हर क्षेत्र में उन्नत था, परंतु सैंकड़ों वर्षों की पराधीनता ने उसे कहाँ से कहाँ से पहुँचा दिया। वह दुर्बल, निर्धन तथा पिछड़ा हुआ देश बनकर रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। परंतु स्वाधीन होने के इतने वर्षों बाद भी मानसिक रूप से हम स्वाधीन नहीं हो पाए। विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता और विदेशी भाषा को अपनाकर आज भी हम अपनी मानसिक पराधीनता का परिचय दे रहे हैं।
लाला लाजपतराय पराधीनता के युग में विदेश यात्रा पर गए। हर जगह उनका स्वागत हुआ। लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। अपने देश को स्वाधीन करने के लिए उन्होंने विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। जब वे भारत आए तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि वे अनेक देशों मे घूमे, पर हर स्थान पर भारत की पराधीनता का कलंक उनके माथे पर लगा रहा।
हमारा कर्तव्य है कि हम कभी भी राजनैतिक, सांस्कृतिक या किसी अन्य प्रकार की पराधीनता स्वीकार न करें। हर राष्ट्र के लिए स्वाधीनता का बहुत अधिक महत्त्व है। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है, यदि वह स्वाधीन हो। जो जाति अथवा देश स्वाधीनता का मूल्य नहीं पहचानता तथा स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह एक-न-एक दिन
पराधीन अवश्य हो जाता है तथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्वाधीनता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कवि दिनकर ने कहा है-
‘स्वातंत्र्य जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है,
बाहरी वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है।
नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है,
स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है।’
23. का बरषा जब कृषि सुरवाने
अथवा
समय का सदुपयोग
संकेत : समय अमूल्य वस्तु, समय का महत्त्व, कार्य की सफलता, छात्रावस्था में समय का महत्त्व, उपसंहार।
संसार में समय को बहुमूल्य वस्तु माना गया है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण दुर्लभ संपत्ति है क्योंकि धन-दौलत यदि नष्ट हो जाए तो उसे परिश्रम करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु समय वह संपत्ति है, जिसे खो जाने या नष्ट हो जाने पर दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग मानव के लिए बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही काम करना ही समय का सदुपयोग है।
‘अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत’
उक्ति में भी समय के महत्त्व को उजागर किया गया है। समय का सदुपयोग करने का महत्त्व बताया है। साथ ही सावधान भी किया गया है कि यदि समय पर कर्म करने से चूक जाओगे, समय का सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो बाद में जीवन अभिशाप बन जाएगा। हर व्यक्ति के मन में उन्नति की चाह होती है। वह बलवान, धनवान व विद्वान बनना चाहता है। जब मनुष्य की ऐसी चाहत हो तो उसे समय के सदुपयोग की ओर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि जिसने समय का सदुपयोग किया, वह सफलता की चोटी पर पहुँच गया। गांधी, नेपोलियन, अरस्तू, मैडम क्यूरी आदि महान् लोगों ने समय के महत्त्व को समझा और सफलता प्राप्त की। कहा भी गया है-
‘समय का चूका विद्यार्थी, बरसात का चूका किसान तथा
डाल का चूका बंदर कहीं का नहीं रहता।’
जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। जो समय को नष्ट करता है, समय भी उसे नष्ट कर देता है। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से उनकी सफलता का राज पूछा था। गांधी जी ने मुस्कराते हुए अपनी कमर में लटकी घड़ी की ओर इशारा किया, यानी समय की पाबंदी। गांधी जी ने जीवन-भर बहुत सावधानी तथा बुद्धिमानी से समय का उपयोग किया था, इसीलिए वे विश्व प्रसिद्ध हुए। नेपोलियन ने एक-एक क्षण का सदुपयोग कर अपने शौर्य से यह सिद्ध कर दिया कि उसके शब्दकोश में असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है।
समय का हर पल, हर क्षण, प्रत्येक सांस ही जीवन है। जिसने एक-एक क्षण का सदुपयोग किया, विजय का सेहरा उसके सिर पर बँधता है और जिसने एक क्षण की चूक की, उसके मुँह पर कालिख लग जाती है। कार्य की सफलता कुशलता से ज़्यादा तत्परता पर निर्भर करती है। यह बहुत सही कहा गया है
‘समय बहुमूल्य है। समय ही धन है। समय पर संपन्न कार्य ही फलदायी होता है।’
समय ही सत्य है। उसका सदुपयोग ही सफलता और समृद्धि का प्रतीक व परिचायक है। समय का सदुपयोग हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित जीवन जीना चाहिए। आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति ये दोनों समय के दुश्मन हैं। जैसे कि कहा गया है
समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते।’
हमारे देश में समय का दुरुपयोग बहुत होता है। बेकार की बातों में समय व्यर्थ गँवाया जाता है। मनोरंजन के नाम पर भी समय बेकार किया जाता है। समय को खोकर कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता।
छात्रावस्था में भी समय का बहत महत्त्व है। जो छात्र प्रतिदिन की अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं कर पाते, उन्हें परीक्षा के समय पाठ्यक्रम पहाड़ के समान जटिल प्रतीत होता है और तब परीक्षा में सफलता के लिए वे गलत हथकंडे अपनाते हैं। इन गलत कामों से भी उन्हें असफलता ही हाथ लगती है और समाज के सामने उनका सिर नीचा होता है। वे बाद में पछताते हैं, लेकिन पछताने से क्या लाभ, क्योंकि कहा भी गया है
“का बरखा जब कृषि सुखाने।
समय चूकि पुनि का पछताने।”
प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक क्षण का सदुपयोग कर छात्रावस्था में विद्यार्जन, युवावस्था में धनार्जन तथा प्रौढ़ावस्था में ज्ञानार्जन करना चाहिए, अन्यथा वृद्धावस्था में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
हमें सदा अपने कार्य निश्चित समय में ही पूरे करने चाहिएँ। हम भारत के नागरिक अपने देश के निर्माता हैं। अपनी तथा अपने देश की उन्नति के लिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम सब कार्य निश्चित समय में करेंगे तो अतिरिक्त समय भी बच जाता है, जिसमें हम समाज-कल्याण में कार्य कर सकते हैं। कबीर जी ने भी कहा था कि आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए
‘काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होयगी, बहुरि करैगो कब।’
हमें सदा यह प्रयास करना चाहिए कि समय व्यर्थ न चला जाए। समय का भरपूर उपयोग करना तथा समय के मूल्य को पहचानना ही सफलता प्राप्ति का मूलमंत्र है।

24. महिला सशक्तीकरण
नारी आदिकाल से माँ, बहन, पत्नी, मित्र आदि अनेक रूपों में मानव-समाज के सामने आती रही है। पुरुष और महिला फिर जीवन-रूपी रथ के दो समान पहिए हैं। उनमें से किसी एक के बिना जीवन अधूरा रह जाता है नारी पत्नी के रूप में परामर्शदात्री और माँ के रूप में हमारी गुरु है। इसलिए जीवन-रूपी रथ को चलाने के लिए उसके दोनों पहिए अर्थात् पुरुष एवं महिला दोनों का समान महत्त्व है। दोनों का सबल होना अनिवार्य है।
महिला वर्ग की स्थिति को सुधारने हेतु उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में उनमें अज्ञानता पैदा हो गई, जिसके कारण गृहस्थ जीवन के चित्र कुरूप होने लगे। अज्ञानता के कारण ही स्त्रियों में हीन भावना उत्पन्न हो गई तथा उस पर तरह-तरह के अत्याचार होने लगे, किन्तु आधुनिक युग में इस बात को अनुभव किया गया कि यह सब शिक्षा के अभाव में ही हुआ है। इस स्थिति से बचने के लिए महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना अनिवार्य है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु महिलाओं का ज्ञानवान् होना अनिवार्य है। शिक्षा ग्रहण करके आज महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के समान लागे बढ़ रही हैं। आज महिला योग्य डॉक्टर, योग्य नर्स, योग्य प्रशासिका, योग्य प्राध्यापिका, योग्य व्यवस्थापिका, यहाँ तक कि कुशल पुलिस अधिकारी और सेनानायिका आदि हैं।
आज भारत में नारी को संविधान द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे पूर्व नारी को पुरुष ने अपने समान नहीं समझा था। आज नारी को न केवल मतदान करने का ही अधिकार दिया गया है अपितु उसे हर क्षेत्र में बड़े-से-बड़े पद पर आसीन होने पर समान अधिकार है। आज नारी पुरुष के समान जिला परिषद्, नगर परिषद् विधानसभा, लोकसभा आदि सभी छोटे-बड़े चुनाव में भाग ले सकती है। इसी प्रकार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त हैं इससे महिला समाज में न केवल आत्म-सम्मान ही बढ़ा, अपितु इसमें नवचेतना भी जागृत हुई है जिसके बल पर महिला वर्ग आज नए-नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है।
जीवन में न्याय मिलना अति अनिवार्य है। महिलाओं के सन्दर्भ में तो यह बात और भी अधिक अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि हमारे समाज में महिला-वर्ग के प्रति अत्यधिक शोषण, अन्याय और अत्याचार होते रहे हैं। आज भी स्वतन्त्र भारत में महिलाओं को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाता। पुरुष-प्रधान समाज में कदम-कदम पर महिलाओं पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है न्याय की दृष्टि से पुरुष और महिला को समान समझा जाना चाहिए। न्याय की दृष्टि से महिला वर्ग के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। आज़ नारियों को दहेज न लाने के कारण अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया जाता है या जीवित ही जला दिया जाता है। ऐसा कुकर्म करने वाले व्यक्ति को कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
महिलाओं को पुरुषों के समान विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। विचार लिखकर व बोलकर ही व्यक्त किए जा सकते हैं। वह राष्ट्र ही सभ्य अथवा उन्नत कहा जा सकता है जहाँ हर नागरिक को लिखने व भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। महिलाओं को यदि बोलकर या लिखकर भाषण देने का अधिकार नहीं होगा तो उनका बौद्धिक विकास सम्भव नहीं होगा। बुद्धि और प्रतिभा का विकास न होने के कारण वे अनेक प्रकार की कुरूपताओं से ग्रस्त हो जाएँगी। अतः महिला-वर्ग को विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए।
महिलाओं को सामाजिक स्वतन्त्रता का अधिकार भी मिलना अनिवार्य है। हमारे समाज में महिला-वर्ग पर अनेक सामाजिक अन्याय व अत्याचार किए जाते रहे हैं। उसे पुरुष की इच्छानुसार पर्दा-प्रथा का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार विवाह को लेकर उसके साथ सामाजिक अन्याय किया जाता है। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया जाता है उसके सम्बन्ध में महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक स्वतन्त्रता के अभाव में नारी का जीवन अत्यन्त कष्टमय बन जाता है। नारी का जीवन सामाजिक न्याय एवं स्वतन्त्रता के अभाव में अत्यन्त कष्टमय बन जाता है। स्वतन्त्रता का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वह अपनी इच्छानुसार विवाह कर सके और अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके।
आज का युग स्वतन्त्रता का युग है। संविधान की ओर से सभी नागरिकों को राजनीतिक स्वतन्त्रता का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को भी राजनीति में सक्रिय भाग लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन्हें राजनीति में भाग लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ताकि वे, विधान सभा और लोकसभा में जाकर महिलाओं के पक्ष में आवाज उठा सकें, उनके अधिकारों की सुरक्षा कर सकें और उन पर हो रहे तरह-तरह के अत्याचारों को सामने ला सकें। भारतवर्ष में इस क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए हैं, आज ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक में महिला वर्ग के स्थान सुरक्षित हैं।
25. महंगाई की समस्या
संकेत : भूमिका, मुद्रास्फीति और महँगाई, भारत में महंगाई के कारण, जमाखोरी की समस्या, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, महँगाई को रोकने के उपाय, समुचित वितरण की व्यवस्था, उपसंहार।
बढ़ती हुई महँगाई देश की अनेक समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। ज्यों-ज्यों सरकार महँगाई को रोकने का आश्वासन देती जा रही है, त्यों-त्यों महँगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। जनता बार-बार सरकार से आग्रह करती है कि वह उचित मूल्यों पर. आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराए लेकिन उचित मूल्यों की बात तो दूर रही, अनेक बार आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ भी बाज़ार से लुप्त ही हो जाती हैं।
इस बढ़ती हुई महँगाई का संबंध प्रत्यक्षतः मुद्रा-स्फीति के साथ है। सरकार प्रतिवर्ष घाटे का बजट बढ़ाती जाती है, उधर कीमतें बढ़ती जाती हैं। परिणाम यह होता है कि रुपए की कीमत भी घटती जाती है। महँगाई भत्ता तो एक नियमित प्रक्रिया बन गई है। सरकारी कर्मचारी हों या गैर-सरकारी-सभी महँगाई भत्ते की माँग करते हैं। सरकार नोट छापकर मुद्रा फैलाती है। इस प्रकार से यह चक्र निरंतर चलता रहता है।
महँगाई की समस्या का शिकार केवल हमारा देश ही नहीं है अपितु संसार के सभी विकासशील देश इसके शिकार बने हुए हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये देश भी महँगाई पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।
भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में इसका स्थान दूसरा है। हमारे देश में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से उपज नहीं। पिछले दो-तीन दशकों में उपज में आशातीत वृद्धि हुई है लेकिन उधर प्रतिवर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पैदा हो रहा है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि आदि के कारण भी अनाज में कमी आ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमें अनेक बार विदेशों से अनाज का आयात करना पड़ता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश की समूची अर्थव्यवस्था अच्छी वर्षा पर निर्भर करती है। बिजली उत्पादन भी इसे प्रभावित करता है।
महँगाई का एक बड़ा कारण वस्तुओं की जमाखोरी है। हमारे देश के पूँजीपति इस महँगाई के लिए सर्वाधिक दोषी हैं। जब-जब मंडियों में अनाज आता है, तब-तब लोग उसे खरीदकर अपने गोदामों में भर लेते हैं। इसी प्रकार से वे अन्य वस्तुओं का भी संग्रह कर लेते हैं। फलस्वरूप, आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं। इस प्रकार, व्यापारी दुगुने-तिगुने दामों पर अपना माल बेचता है। जब-जब देश में सूखा पड़ा है, व्यापारियों ने खूब हाथ रंगे हैं। यद्यपि सरकार की ओर से इस प्रकार की अव्यवस्था के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं तथापि भ्रष्ट अधिकारी वर्ग व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी सहायता करता रहता है।
आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के समुचित वितरण के लिए आवश्यक कानून बनाए गए हैं। प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न आपूर्ति विभाग स्थापित किए गए हैं। स्थान-स्थान पर राशन की दुकानें भी खोली गई हैं। यदि खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था समुचित हो तो महँगाई पर नियंत्रण किया जा सकता है परंतु यह सब हो नहीं पाता। व्यापारी वर्ग का लक्ष्य अधिकाधिक धन कमाना है और वह इसके लिए नए-नए रास्ते निकालता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार का अजगर यहाँ भी अपना काम करता रहता है। वस्तुओं की वितरण-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। परिणाम यह होता है कि दुकानदार आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का संग्रह कर लेता है जिससे मूल्य बढ़ते रहते हैं।
प्रयत्न किया जाए तो इस महँगाई को रोका भी जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार मुद्रा-स्फीति पर रोक लगाए और प्रतिवर्ष घाटे का बजट न बनाए। कृषि उत्पादन और दुग्ध उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित करने होंगे। हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश के किसानों को सिंचाई की पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को बड़े-बड़े नगरों के विकास के स्थान पर गाँवों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। सारे देश के लिए एक ही प्रकार की सिंचाई-व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए।
अनेक बार ऐसा भी देखने में आता है कि अच्छे उत्पादन के बावजूद भी वस्तुएँ नहीं मिलती अथवा मिलती भी हैं तो महँगी। इसके लिए हमारी वितरण-व्यवस्था दोषी है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण आ चुके हैं जो सिद्ध करते हैं कि भ्रष्ट व्यापारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से महँगाई बढ़ती रहती है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। व्यापारियों को मनमानी करने का मौका तो कभी नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार की वस्तुओं के वितरण के कार्य को सरकार अपने हाथ में ले और ईमानदार अधिकारियों को यह काम सौंपे।
इसके लिए आज एक उपयोगी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ महँगाई पर रोक लगाना ज़रूरी है अन्यथा हमारी स्वतंत्रता के लिए पुनः खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण है। जब तक इस पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे।

26. भारतीय संस्कृति एवं विश्व
भारतीय संस्कृति और विश्व अथवा भारतीय संस्कृति की विश्व को देन जैसे विषय पर विचार करने से पूर्व ‘संस्कृति’ शब्द का अर्थ समझ लेना अनिवार्य है क्योंकि आजकल संस्कृति और सभ्यता को एक-दूसरे का पर्याय समझने लगे हैं। इसलिए संस्कृति को लेकर अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। सत्य यह है कि संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग-अलग होती हैं किन्तु हैं एक-दूसरे के करीब। वस्तुतः सभ्यता का सम्बन्ध हमारे बाहरी जीवन के ढंग व तौर-तरीके से है; जैसे खान-पान, रहन-सहन, बोलचाल, जबकि संस्कृति का सम्बन्ध मानवीय सोच, चिन्तन-मनन, विचारधारा से है। संस्कृति का क्षेत्र सभ्यता की अपेक्षा अधिक विस्तृत और गहन है। सभ्यता का अनुकरण तो सहज ही किया जा सकता है, किन्तु संस्कृति का नहीं। हम पैंटकोट पहनकर व अंग्रेज़ी बोलकर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर सकते हैं किन्तु वहाँ की संस्कृति का नहीं।
संस्कृति किसी भी देश की आत्मा होती है। संस्कृति से ही किसी देश व जाति के उन सभी संस्कारों का बोध होता है जिनकी सहायता से वह अपने आदर्शों और जीवन-मूल्यों का निर्धारण करता है। ‘संस्कृति’ शब्द का अर्थ है-संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी संस्कृति का अर्थ संस्कार ही स्वीकार किया गया है। आज भले ही अंग्रेज़ी शब्द ‘कलचर’ का प्रयोग संस्कृति के समानान्तर किया जाने लगा है, किन्तु वास्तविकता तो यह है संस्कृति का सम्बन्ध मानवीय जीवन-मूल्यों से है।
भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व की कई संस्कृतियाँ इसके सामने आईं और चली गईं। भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता की ओर संकेत करते हुए कविवर इकबाल ने लिखा है
“यूनान, मिस्र सब मिट गए जहाँ से,
अब तक मगर है बाकि नामोनिशां हमारा।”
इन काव्य पंक्तियों से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण यह प्राचीनकाल से आज तक निरन्तर चली आ रही है। भारतीय संस्कृति का विश्व को यह सन्देश है कि सदैव जीवित रहने के लिए अपने आप में लचीलापन का गुण उत्पन्न करें। इसी गुण के बल पर कोई संस्कृति समय के साथ-साथ आगे बढ़ सकती है।
भारतीय संस्कृति की अन्य प्रमुख विशेषता है-समायोजन की क्षमता अर्थात् अपनें में समा लेने की क्षमता। भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता के कारण ही भारत में आने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ के होकर रह गए हैं। आज विश्व के अनेक देश हैं जहाँ की संस्कृति में यह क्षमता नहीं है। अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण वे दूसरे धर्म व जाति के लोगों को सहन नहीं कर सकते। फलस्वरूप वहाँ दंगे व अशांति का नग्न ताण्डव देखा जा सकता है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति ने सम्पूर्ण विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यदि उनमें समायोजन की शक्ति व क्षमता हो।
भारतीय संस्कृति की नींव मानव-कल्याण की भावना पर खड़ी है। यहाँ सभी कार्य ‘बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय’ के नियम को सामने रखकर किए जाते हैं। यही भाव भारतीय संस्कृति को आदर्श संस्कृति की पदवी दिलवाता है। भारतीय संस्कृति की उदारता को दर्शाने वाला दूसरा मंत्र है-‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् सारी धरती के लोग एक परिवार की भांति हैं। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता से विश्व को यह शिक्षा मिलती है कि जब सारा संसार एक परिवार है तो फिर तेरे-मेरे की भावना को त्यागकर तथा एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह विश्व स्वर्ग बन जाएगा। सभी लोग सुखी हो जाएंगे। दुःखों का भूत यहाँ से विदाई ले लेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का विश्व को यह सन्देश है कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुःख प्राप्त न हो। भारतीय संस्कृति की ऐसी पुनीत भावनाओं से प्रभावित होकर हर समस्या के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता रहा है।
भारतीय संस्कृति का मूल-मन्त्र आध्यात्मिकता है। भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिकता का आधार ईश्वरीय विश्वास है। यहाँ विभिन्न धर्मों व मतों में विश्वास रखने वाले लोग आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर ही इस सृष्टि का रचयिता और नियन्त्रक है। वही सृष्टि का कारण, पालक और संहारकर्ता है। भारतीय संस्कृति की इस विशेषता से विश्व को यही संदेश जाता है कि जब सबका रचयिता एक है तो फिर अपने-पराए का विचार ही जड़ से समाप्त हो जाता है। संसार के सभी लोग एक परमपिता की संतान हैं। फिर भेद-भाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सम्पूर्ण संसार एक परिवार है।
त्याग व तपस्या भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। भारतीय संस्कृति में त्याग की भावना पर विशेष बल दिया जाता है। त्याग के कारण ही मानव-जीवन में सन्तोष जैसे गुण का विकास होता है। भारतीय संस्कृति की इस त्याग की विशेषता से विश्व को यह उपदेश दिया है जहाँ त्याग की भावना है, वहाँ संकट के समय में दूसरों की सहायता की जाती है, वहाँ स्वार्थ व लालच जैसी दुर्भावनाओं का विनाश हो जाता है। आज विश्व में त्याग की भावना न होने के कारण लालच की भावना पनपी है जिससे चारों ओर हाहाकार मची हुई है। सभी एक-दूसरे से छीना-झपटी करने में व्यस्त हैं। कर्ण, हरिश्चन्द्र, दधीचि आदि का त्याग भारतीय संस्कृति का आदर्श नहीं, अपितु पूरे विश्व का आदर्श है। दूसरों के लिए अपने स्वार्थों एवं सुख का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति ने विश्व को सिखाया है कि त्याग में ही जन-कल्याण की भावना का विकास सम्भव है। स्वामी विवेकानन्द ने भी त्याग और सेवा को भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताई है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के इसी रूप को विश्व के समक्ष रखा है।
भारतीय संस्कृति में उन्मुक्त अथवा स्वच्छन्द सुख-भोग का विधान नहीं है। यहाँ हर उपभोग में संयम बरतने का नियम है। उन्मुक्त, सुखभोग से मनुष्य में लालच की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह मनुष्य को असन्तोषी बनाता है। लालची और असंतोषी व्यक्ति कभी शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जब व्यक्ति अपनी कामनाओं अथवा इच्छाओं को कम कर देगा तो उसकी समस्याएँ भी कम हो जाएँगी। यहाँ के संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों ने विश्व को यही सन्देश दिया है कि त्याग और तपस्या से विश्व की भलाई सम्भव है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के धर्म का सम्मान करना और तपस्वी जीवन व्यतीत करना ही मानव का संस्कार होना चाहिए।
आज के वैज्ञानिक युग में सभी देश शांति स्थापित करने के लिए परमाणु बम व हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। दूसरों को डराकर शांति स्थापित करने का यह ढंग बहुत ही खतरनाक है। डर के वातावरण में शांति स्थापित नहीं हो सकती, किन्तु भारतीय संस्कृति के अनुसार, प्रेम, सद्भावना, विश्वास और एक-दूसरे को समझकर कार्य करने से ही शांति की स्थापना हो सकती है। इसलिए आज भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्त ही विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं।
भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर करना, पारिवारिक भावनाओं को बढ़ावा देना, गुरु का सम्मान करना, गुरु-शिष्य में पावन सम्बन्ध आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं जिनसे सामाजिक जीवन का समुचित विकास होता है। आज हर व्यक्ति में अकेलेपन की भावना के घर कर जाने से हर चेहरे पर निराशा झलक रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति यह पाठ पढ़ाती है कि आपस में मिल-जुलकर रहना, एक-दूसरे का सम्मान करना, आपसी सम्बन्धों को समझ के आधार पर मज़बूत बनाए रखना आदि सुखी एवं खुशहाल सामाजिक जीवन के विकास के लिए नितान्त आवश्यक है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति सदैव विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत रही है। भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य ही ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, ‘सर्व हिताय’-‘सर्व सुखाय’ के विचार को विकसित करना है। इसलिए सम्पूर्ण विश्व भारतीयों और भारतीय संस्कृति की ओर आशाभरी दृष्टि से देखता है।

27. प्रदूषण की समस्या
संकेत : भूमिका, प्रदूषण का अर्थ एवं स्वरूप, वायु-प्रदूषण की समस्या, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण से बचने के उपाय, उपसंहार।
आज के वैज्ञानिक युग में मानव-जीवन के सामने अनेक समस्याएँ हैं। विज्ञान ने जहाँ एक ओर सुख-सुविधाएँ उत्पन्न करके मानव-जीवन को सुखी बनाया है, वहाँ मनुष्य के जीवन में अनेक दुःखों को भी जन्म दिया है। अतः विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। आज प्रदूषण विज्ञान का एक प्रमुख अभिशाप है जिसे संसार के अधिकतर लोगों को भोगना पड़ रहा है। प्रदूषण की यह समस्या सारे संसार में फैल चुकी है।
प्रदूषण का अर्थ है प्रकृति के स्वस्थ, सर्वजन-सुलभ कोष में असंतुलन। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाए रखती है परंतु आज विज्ञान ने प्रकृति के संतुलन में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। बड़े-बड़े नगरों में प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक है। इससे मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मोटरों, बसों तथा कल-कारखानों से निकले धुएँ के कारण वायु दूषित हो जाती है। इसी दूषित वायु के कारण फेफड़ों तथा हृदय की अनेक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। आज अनेक बीमारियों का तो मूल कारण ही प्रदूषण है।
जनसंख्या की अधिकता तथा सड़कों, गलियों में वृक्ष न होने के कारण वायु-प्रदूषण बढ़ता है। बाजारों में मोटरों की विषैली वायु निकलने की व्यवस्था न होने के कारण वायु-प्रदूषण स्वाभाविक है। आवासीय तथा व्यापारिक केंद्रों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सड़कें चौड़ी हों, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष हों, पार्क हों ताकि वायु-प्रदूषण कम हो सके। इस प्रकार नगरों का जीवन शुद्ध हो सकता है।
उद्योगों के निरंतर बढ़ने के कारण भी वायु-प्रदूषण बढ़ रहा है। विषैली गैसों, मशीनों से निकले हुए मल से कई बीमारियों का जन्म होता है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए नई योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। जल-प्रदूषण भी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। कारखानों का दूषित जल नदी-नालों में मिलकर सारे जल को खराब कर देता है। वर्षा के दिनों में जल इकट्ठा होकर दुर्गंध पैदा करता है। उस पानी में कीट, मच्छर आदि जीव जन्म लेकर वातावरण को दूषित बना देते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी आज एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुका है। यातायात का शोर, मोटर-गाड़ियों तथा अज्ञानतावश प्रयोग किए जाने वाले लाऊडस्पीकरों की कर्ण-भेदी आवाज़ों ने बहरेपन की समस्या को जन्म दिया है। ध्वनि-प्रदूषण से फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है। मानव के स्वभाव पर भी ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है।
पर्यावरण प्रदूषण के अनेक बुरे परिणाम हैं। खेती के आधुनिक उपायों, खादों तथा कृत्रिम साधनों के प्रयोग के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है। बीज तथा खाद के दूषित होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं तथा इनके सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर अणु बम का दुष्प्रभाव अभी तक वहाँ व्याप्त है। अणु बम के दुष्प्रभाव के कारण वहाँ पर अभी भी लोगों की संतानें विकलांग पैदा हो रही हैं। अणु विस्फोट के कारण मौसम का सारा संतुलन बिगड़ जाता है।
प्रदूषण के कारण आज समूचे देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण चरमरा गया है। दिल्ली जैसे महानगरों में प्रवेश करते ही दम घुटने लगता है और आँखों में जलन होने लगती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली महानगर का प्रत्येक तीसरा नागरिक श्वास-रोग से ग्रसित है। वहाँ पर चलने वाले वाहनों के कारण सारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। लगभग यही स्थिति चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, मुंबई आदि नगरों की है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि प्रदूषण के कारण हमारा जीवन नरक-तुल्य हो गया है। रोग बढ़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। प्रदूषण के कारण हमारे देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने चाहिएँ। आवास की व्यवस्था खुली तथा हवादार होनी चाहिए। हरियाली बनाए रखने के लिए पार्क बनाने चाहिएँ। सड़कें चौड़ी होनी चाहिएँ ताकि गंदी वायु निकलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों तथा धुएँ के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वर्षा के पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमारे देश में प्रदूषण को रोकने के जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में बने प्रदूषण बोर्डों के कर्मचारी इस दिशा में अधिक प्रयत्नशील नज़र नहीं आते। उन पर तरह-तरह के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव डाले जाते हैं। जनता में भी इस संबंध में जागरूकता की नितांत आवश्यकता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण तो बढ़ती हुई जनसंख्या है। जब तक इस पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक हम प्रदूषण की समस्या पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
रूस और अमेरिका जैसे बड़े-बड़े देशों ने प्रदूषण समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्रदूषण रोकने में उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। भारत को भी समय रहते प्रदूषण से बचने के उपाय करने चाहिएँ ताकि इस गंभीर समस्या को समाप्त किया जा सके तथा मानव-जीवन को स्वस्थ बनाया जा सके।

28. आतंकवाद की समस्या
अथवा
विश्वव्यापी आतंकवाद
संकेत : भूमिका, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के मूल कारण, सांप्रदायिकता का ज़हर, दूषित राजनीति, युवकों में बेरोज़गारी, आतंकवाद रोकने के उपाय, उपसंहार।
आतंकवाद आधुनिक युग की सर्वाधिक भयंकर समस्या है। यह समस्या केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह समूचे संसार में फैल चुकी है। निरपराध और निरीह लोगों की निर्मम हत्या, बम विस्फोट, हवाई जहाज़ों का अपहरण, रेल की पटरियों को उखाड़ना, बैंकों को लूटना, बसों को जलाना, यात्रियों को मारना आदि अनेक हिंसापूर्ण कार्य आतंकवाद के नाम पर हो रहे हैं। यही नहीं, आतंकवादियों ने अपने-अपने गिरोह बना रखे हैं और वे किसी भी देश की कानून-व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। वे मनमाने ढंग से लोगों की हत्याएँ करते रहते हैं।
‘आतंकवाद’ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है-‘आतंक’ और ‘वाद’ । ‘आतंक’ का अर्थ है-भय या डर। ‘वाद’ का अर्थ हैपद्धति। आतंकवादियों का एक ही लक्ष्य है-सरकार और लोगों के दिलों में भय उत्पन्न करके अपनी अनुचित बातों को मनवाना। आतंकवादियों का कोई धर्म, जाति या देश नहीं होता। ये भोले-भाले बच्चों, निरीह स्त्रियों, बूढ़ों और जवानों सभी की हत्या कर देते हैं। कानून-व्यवस्था को ताक पर रखकर ये देश में अराजकता उत्पन्न करते हैं।
आतंकवाद की समस्या पिछले एक दशक की उपज है। आज से दस वर्ष पहले छिट-पुट रूप में लूटपाट के मामले सभी देशों . में होते थे लेकिन आज इस समस्या ने अजगर का रूप धारण कर लिया है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इसके मूल कारण क्या हैं ? ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, जिनके कारण यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है ? विद्वानों और राजनीति शास्त्रियों ने इस समस्या पर विचार करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं।
सांप्रदायिकता इसका प्रमुख कारण है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोगों का वर्ग भी है जो स्वतंत्रता के बाद भी संकीर्ण और कट्टर धार्मिक विचारधारा के शिकार बने हुए हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्मों के प्रति असहज हो जाते हैं। पुन: ये लोग धर्म और राजनीति को मिलाने का प्रयास करते हैं। ये धर्म के नाम पर अलग राज्य बनाना चाहते हैं। जो लोग उनकी धार्मिक परिधि में नहीं आते, उनके प्रति वे घृणा की भावना फैलाते हैं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावना ही आतंकवाद को जन्म देती है। जो लोग एक संप्रदाय के प्रति समर्पित हैं, वे दूसरे संप्रदायों के लोगों से घृणा करते हैं।
हमारे देश की असंख्य समस्याओं के लिए आज की दूषित राजनीति बहुत कुछ उत्तरदायी है। हमारे राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक पार्टियाँ धर्म एवं जाति के नाम पर लोगों को भड़काती हैं और अपने वोट पक्के करती हैं। आज भी चुनावों के अवसर पर धर्म या जाति के नाम पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। कालांतर में जो लोग संकीर्ण और कट्टर बन जाते हैं, वही आतंकवादी बन जाते हैं। 11 सितंबर, 2001 मंगलवार को उग्रवादियों ने न्यूयार्क स्थित विश्व व्यापार संगठन कार्यालय के दो टावरों एवं अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रमुख कार्यालय पेंटागन के कुछ क्षेत्र को यात्री विमानों द्वारा टक्कर मारकर ध्वस्त कर दिया। अमेरिका में यह संसार की सबसे बड़ी विनाशकारी दुर्घटना मानी जाती है जिससे हज़ारों निरीह लोगों की जानें चली गईं। हमारे अपने देश में पिछले दो दशकों में अकेले कश्मीर में 55 हज़ार निर्दोष लोग उग्रवादियों के आतंकवाद के शिकार बन चुके हैं। इसी प्रकार, 13 दिसंबर, 2001 को संसार के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक राज्य दिल्ली के संसद भवन में आतंकवादियों ने आत्मघाती आक्रमण करके अपनी अमानवीयता का परिचय दिया है।
आतंकवाद की लपेट में जितने भी लोग आए हैं, वे प्रायः बेरोज़गार और अर्द्धशिक्षित युवक हैं। आतंकवाद की रीति-नीति चलाने वाले लोग इन बेरोजगार युवकों को अपने चंगुल में फँसा लेते हैं। जब कोई युवक अपराधी बन जाता है, तब उसके लिए उग्रवाद की चपेट से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। चूँकि युवकों का मन और मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, उन्हें किसी भी साँचे में ढाला जा सकता है। जिस प्रकार के लोग उनके साथ रहते हैं, वे उसी प्रकार के बनते हैं। पंजाब में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनमें से अधिकांश ने बेरोज़गारी से तंग आकर ही यह रास्ता अपनाया।
आतंकवाद मानवता के नाम पर कलंक है। यह किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है-स्वयं आतंकवादियों के लिए भी नहीं। इससे मानवता की काफी हानि हो चुकी है। आतंकवाद रूपी दानव ने न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया है, कितनी स्त्रियों को विधवा बना दिया है और न जाने कितने लोगों को बेसहारा बना दिया है। सर्वप्रथम, सरकार को उग्रवादियों के साथ कठोर कार्रवाई करनी होगी। अपनी सीमाओं पर कड़ी चौकसी करने की आवश्यकता है। जो युवक उग्रवाद की चपेट में आ चुके हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाकर किसी उपयोगी रोजगार से जोड़ना होगा। इसी प्रकार से लोगों में देशप्रेम की भावना को उत्पन्न करना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता को भी समाप्त किया जाना चाहिए।
हमारा देश शांति और अहिंसा की जन्म-भूमि है। यहाँ महात्मा बुद्ध और गांधी जैसे मानवता प्रेमियों का जन्म हुआ है। अतः महान ऋषियों, मुनियों, संतों और गुरुओं की वाणी का प्रचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी का भी कर्तव्य है कि वह संकीर्णता के दायरे से बाहर निकल परस्पर धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करे, तभी यह आतंकवाद समाप्त होगा।
30. भ्रष्टाचार-कारण व निवारण
संकेत : भूमिका, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के मूल कारण, भ्रष्टाचार की व्यापकता एवं प्रभाव, भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय, उपसंहार।
किसी भी देश के विकास के मार्ग में उस देश की विभिन्न समस्याएँ बहुत बड़ी बाधा हैं। इन समस्याओं में प्रमुख समस्या है-भ्रष्टाचार की समस्या। जिस समाज व राष्ट्र को भ्रष्टाचार का कीड़ा ग्रसने लगता है, उसका भविष्य फिर निश्चित रूप से अंधकारमय बन जाता है। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि उस पर यह समस्या पूर्ण रूप से छाई हुई है। यदि समय रहते इसका समाधान न ढूँढा गया तो इसके भयंकर परिणाम सामने आएँगे।
भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है-आचार से भ्रष्ट या अलग होना। अतः कहा जा सकता है कि समाज स्वीकृत आचार-संहिता की अवहेलना करके दूसरों को कष्ट पहुँचाकर निजी स्वार्थों अथवा इच्छाओं की पूर्ति करना ही भ्रष्टाचार है। दूसरे शब्दों में, भ्रष्टाचार वह निंदनीय आचरण है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। भाई-भतीजावाद, बेरोज़गारी, गरीबी आदि इसके दुष्परिणाम हैं जो हमारे राष्ट्र को भोगने पड़ रहे हैं।
प्रत्येक विकराल समस्या के पीछे कोई-न-कोई कारण अवश्य रहता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार के विकास के पीछे भी विभिन्न कारण हैं। वस्तुतः सुख एवं ऐश्वर्य के पनपने के साथ-साथ भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार के मूल में मनुष्य का कुंठित अहंभाव, स्वार्थपरता, भौतिकता के प्रति आकर्षण, अर्थ एवं काम की प्राप्ति की लिप्सा छिपी हुई है। मनुष्य की अंतहीन इच्छाएँ भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त, अपनों का पक्ष लेना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। कवि हर्ष ने अपनी रचना ‘नैषधचरितं’ में लिखा है कि अपने प्रियजनों के लिए पक्षपात होता ही है। यही पक्षपात भ्रष्टाचार का मूल कारण है।
भ्रष्टाचार का प्रभाव एवं क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें न फैला रखी हों। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जगत इसकी गिरफ्त में आए हुए हैं। यह घट-घट, कण-कण में राम की भाँति समाया हुआ है। ऐसा लगता है कि संसार का कोई कार्य इसके बिना पूरा नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र तो भ्रष्टाचार का घर ही बन चुका है। आज विधायक हो या सांसद बाज़ार में रखी वस्तुओं की तरह बिक रहे हैं। भ्रष्टाचार के बल पर सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं।
मंदिर का पुजारी भी आज भक्त की स्थिति देखकर पुष्प डालता है। धार्मिक स्थलों पर जाकर देखा जा सकता है कि धर्मात्मा कहलाने वाले लोग ही भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकियाँ लगा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार ने कमाल ही कर दिखाया है। करोड़ों की रिश्वत लेने वाला व्यक्ति सीना तानकर चलता है। अरबों रुपयों का घोटाला करने वाला नेता जनता में सम्माननीय बना रहता है। चुरहट कांड, बोफोर्स कांड, मंदिर कांड, मंडल कांड, चारा कांड आदि सब भ्रष्टाचार के ही भाई-बंधु हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार अपने जौहर दिखा रहा है। योग्य छात्र उच्च कक्षाओं में प्रवेश नहीं पा सकते किंतु अयोग्य छात्र भ्रष्टाचार का सहारा लेकर कहीं-से-कहीं जा पहुँचते हैं और योग्य विद्यार्थी हाथ मलता रह जाता है।
भ्रष्टाचार को रोकना अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि जो-जो कदम इसे रोकने के लिए उठाए जाते हैं, वे कुछ दूर चलकर डगमगाने लगते हैं और भ्रष्टाचार की लपेट में आ जाते हैं। यह संक्रामक रोग की भाँति है। यह व्यक्ति से आरंभ होकर पूर्ण समाज को ग्रस लेता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज में पुनः नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी होगी। जब तक हमारे जीवन में नैतिकता का समावेश नहीं होगा, तब तक हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं बदल सकता। नैतिकता के अभाव में सारी बातें कोरी कल्पना ही बनकर रह जाएँगी। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नैतिकता के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान उत्पन्न करना होगा।
समाज में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उन्हें देखकर दूसरे उनका अनुकरण करने लगे और ईमानदारी के प्रति लोगों के मन में आस्था उत्पन्न हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज दंड व्यवस्था इस तरह कमज़ोर है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो रिश्वत देकर बच निकलता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
भ्रष्टाचार को समाप्त करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति, समाज और संस्था का भी कर्तव्य है। आज हम सबको मिलकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ के सिद्धांत को अपनाकर चलना चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकेंगे। यह बात दो टूक कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार के दानव को नष्ट किए बिना हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार के कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। यह आर्थिक विषय कभी भी देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती है।

31. साम्प्रदायिक सद्भाव
जिस समय भारत में सांप्रदायिक एकता थी, उस समय भारत का विश्व पर शक्ति में, शिक्षा में और शांति में एकछत्र आधिपत्य था। विश्व हमारी ओर आदर की दृष्टि से देखता था। हम विश्व के आदिगुरु समझे जाते थे। भारतीय जीवन के आदर्शों से विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। संपूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में बँधा हुआ था। भारत विश्व में सर्वोत्तम राष्ट्र समझा जाता था। वेदों में भी भारतवासियों को एकता का संदेश देते हुए कहा गया है-तुम सब मिलकर चलो, संगठित हो जाओ, एक साथ मिलकर बोलो। तुम्हारे मन समान विचार वाले हों। जैसे देवता मिलजुल कर विचार प्रकट करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मिलजुल कर रहो।
परन्तु जब से हमारी एकता अनेकता में छिन्न-भिन्न हो गई, तब से हमें ऐसे दुर्दिन देखने पड़े जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें पराधीन होना पड़ा। हमें अपने धर्म एवं संस्कृति पर कुठाराघात सहन करना पड़ा। फलस्वरूप, हमारा राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो गया। हमारी सूत्रबद्ध सामूहिक शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हम अनेक वर्षों तक के लिए गुलामी की जंजीरों में बाँध दिए गए। उन जंजीरों से मुक्त होने की कल्पना भी संदिग्ध प्रतीत होने लगी थी। अनेक बलिदानों के पश्चात बहुत कठिनाई से हमें यह आज़ादी मिली है। सहस्रों वर्षों की परतंत्रता के बाद बड़े भाग्य से हमें ये दिन देखने को मिले हैं। इस आत्म-गौरव को प्राप्त करने के लिए हमें कितना मूल्य चुकाना पड़ा, कितनी यातनाएँ सहन करनी पड़ी। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को कितने भयानक थपेड़े सहन करने पड़े और फिर भी हमारी संस्कृति साँस लेती रही। सैकड़ों वर्षों की अनंत साधनाओं के बाद हमें जो अमूल्य स्वतंत्रता मिली है, हम उसे बरबाद करने में लगे हुए हैं।
आज भारतवर्ष स्वतंत्र है। यहाँ हमारा अपना शासन है किंतु फिर भी सांप्रदायिक एकता अथवा राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएँ आ खड़ी हुई हैं। धर्म, जाति और प्रांत के नाम पर स्थान-स्थान पर लोग आपस में लड़-झगड़ रहे हैं। आज हमारे समाज में कुछ ऐसी ज़हरीली हवा चल रही है कि सब अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलाप रहे हैं। अपने स्वार्थ में डूबे लोग यह भी नहीं सोचते कि जिसके कारण हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है, वह ही नहीं रहेगा अथवा खतरे में पड़ जाएगा तो न हमारी भाषा बचेगी और न हमारा धर्म तथा न जाति। प्रांतीयता के भाव का यह विष अब शनैः-शनैः फैलता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही प्रांत के विषय में सोचता है। बंगाली बंगाल की, मद्रासी मद्रास की, गुजराती गुजरात की तथा पंजाबी पंजाब की उन्नति चाहता है। किसी को भी न तो समूचे राष्ट्र का ध्यान है और न ही कोई अपना दायित्व समझना चाहता है।
हमारे देश में भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। प्रत्येक प्रांत का निवासी अपने प्रांत की भाषा को प्रमुखता देता है। दक्षिणी भारत के कुछ स्थानों पर राष्ट्रगीत इसलिए नहीं गाया जाता क्योंकि वह हिंदी में है। कोई गीता के श्लोकों और रामायण की चौपाइयों को इसलिए मिटा रहा है क्योंकि वे हिंदी में या हिंदी वर्णमाला में हैं। स्वार्थ भावना में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि स्वार्थी नागरिक केवल अपने तक ही सोचता है, अपना कल्याण और अपनी उन्नति ही उसका ध्येय है। न उसे देश की चिंता है, न राष्ट्र की। विभिन्न भाषाओं के साथ-साथ भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों का वास है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत सरकार किसी भी धर्म को आश्रय नहीं देती परन्तु हर धर्म का आदर करती है। लोग केवल अपने-अपने धर्म से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से नहीं। धार्मिक संकीर्णता के कारण जहाँ-तहाँ दंगे होते हैं।
पराधीन भारत में सर्वत्र सांप्रदायिक सद्भावना अथवा एकता थी। सभी संप्रदायों के लोगों ने सच्चे मन से, एक-दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और निःस्वार्थ भाव से महान बलिदान देकर भारत को स्वतंत्र करवाया था। उस समय प्रत्येक भारतीय के मुख पर केवल एक ही नारा रहता था-‘हिंदुस्तान हमारा है’ किंतु आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हम आज नारा लगाते हैं-“पंजाब हमारा है, असम हमारा है।” प्रत्येक व्यक्ति पहले अपनी बात सोचता है फिर प्रदेश की तथा बाद में देश की। यह सोच देश की एकता के लिए घातक है। देश में सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसके लिए अपने जीवन का त्याग किया है। महात्मा गांधी ने अपना पूर्ण जीवन ही सांप्रदायिक सद्भावना और एकता के लिए न्योछावर कर दिया है। हमारे संतों ने सदा परस्पर मिलकर रहने का उपदेश दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री आदि नेताओं ने सदैव राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने के प्रयास किए।
प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयासे करे। सांप्रदायिक सद्भावना ही किसी राष्ट्र की एकता एवं मज़बूती का आधार होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वह संकीर्ण भावनाओं को त्यागकर समूचे समाज अथवा राष्ट्र के लिए सोचे, मनन करे और उसकी समृद्धि के लिए प्रयास करे। यदि समय रहते इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाया गया तो सांप्रदायिक भावना के कारण समाज बिखर जाएगा और राष्ट्र की एकता टूट जाएगी। सशक्त एवं सुदृढ़ राष्ट्र के लिए सांप्रदायिक एकता और सद्भावना का होना नितांत आवश्यक है।
32. मेरा प्रिय लेखक (प्रेमचन्द)
संकेत : भूमिका, जीवन-परिचय, रचनाएँ, भाषा, उपसंहार।
साहित्य समाज का दर्पण है और लेखक युगद्रष्टा होता है। वह अपने आस-पास की परिस्थितियों से प्रेरित होकर साहित्य की रचना करता है। महान् लेखक ही महान् साहित्य की रचना कर सकते हैं। श्रेष्ठ साहित्य का मूल उद्देश्य सत्यम् शिवम् सुन्दरम् होता है। प्रेमचंद महान् कथाकार हैं। उन्होंने अपने युग की परिस्थितियों को समझा, परखा और उन पर गहन चिंतन किया। अपने चिंतन के प्रकाश में उन्होंने युगीन जीवन को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करने के लिए उपन्यास, कहानी, नाटक व निबन्ध साहित्य की रचना की है। उनके उपन्यास इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रत्येक आलोचक ने भी उनके विषय में ऐसा ही मत व्यक्त किया है। हिन्दी उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का आगमन एक शुभ वरदान से कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता।
स्वर्गीय प्रेमचन्द का जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस के समीप लमही नामक एक छोटे से गाँव में सन् 1880 में हुआ। वे अभी छोटे ही थे कि उनकी माता का देहान्त हो गया। पिता ने दूसरा विवाह करने की गलती कर ली। फलस्वरूप घर की परिस्थिति पहले से भी विकट हो गई। प्रेमचन्द का असली नाम धनपतराय था किन्तु इनके चाचा इन्हें नवाबराय कहते थे। इन्हें स्कूल की पढ़ाई के समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अभी पढ़ ही रहे थे कि पिता का स्वर्गवास हो गया। फलस्वरूप सौतेली माँ और उसके बच्चों का दायित्व भी इन्हीं पर आ पड़ा। स्कूल की पढ़ाई जैसे-तैसे पूरी हुई। बाद में एक वकील के बेटे को ट्यूशन । पढ़ाने का काम करने लगे। पाँच रुपए मासिक वेतन के लिए उन्हें कई मील पैदल चलना पड़ता था।
मैट्रिक की परीक्षा के बाद इन्टरमीडिएट में प्रवेश ले लिया किन्तु गणित की अनिवार्यता के कारण परीक्षा पास न कर सके। एक दयालु हैडमास्टर की कृपा से स्कूल में 18 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक हो गए। बाद में बी.ए. तक की पढ़ाई की तथा स्कूल के निरीक्षक के पद तक पहुँच गए किन्तु राष्ट्रीय चेतना व देश-प्रेम के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। प्रैस लगाई, पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की, कहानी लेखक के रूप में फिल्मों में भी रहे किन्तु कहीं स्थायित्व नहीं मिला। दो बार विवाह किया। पहली पत्नी से निर्वाह न होने के कारण अलग हो गए। उस युग में विधवा शिवानी से विवाह करके भारतीय समाज में एक नया आदर्श स्थापित किया तथा दो पुत्रों के पिता बने। सन् 1936 में इस महान् लेखक व साहित्यकार का देहान्त हो गया।
प्रेमचन्द पहले नवाबराय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे किन्तु ‘सोजे वतन’ नामक कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लेने के पश्चात् प्रेमचन्द के नाम से हिन्दी में लिखने लगे। इसी नाम से हिन्दी जगत में प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने दर्जन भर उपन्यास और लगभग तीन-सौ कहानियाँ लिखीं। ‘प्रतिज्ञा’, ‘वरदान’, ‘सेवासदन’, ‘निर्मला’, ‘गबन’, ‘कर्मभूमि’, ‘गोदान’ और मंगलसूत्र (अधूरा) इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में गाँधी युग के समूचे जीवन और घटनाक्रम को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इनके उपन्यासों का प्रमुख स्वर आदर्शवादी रहा है। कुछ आलोचक इन्हें आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी मानते हैं। ‘गोदान’ और ‘मंगलसूत्र’ में लगता है कि ये समाजवादी बन गए थे। इन्होंने हिन्दी उपन्यास को कला और विषय-वस्तु की दृष्टि से नई दिशा दी है। उपन्यास को कल्पना-लोक से निकालकर यथार्थ जीवन से जोड़ दिया है।
प्रेमचन्द की कहानियाँ ‘मानसरोवर’ नामक आठ संग्रहों में संकलित हैं। पंच परमेश्वर, ईदगाह, आत्माराम, बूढ़ी काकी, पूस की रात, बड़े भाई साहब, कफन, शंतरज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी आदि प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उपन्यासों की भांति कहानियों में भी जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। आरम्भिक कहानियाँ आदर्शोन्मुखी हैं। उपन्यास तथा कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचन्द ने दो पाठ्य नाटकों की भी रचना की है। समय-समय पर ये साहित्य, जीवन, समाज आदि से सम्बन्ध रखने वाले विचार प्रधान निबन्ध भी रचते रहे हैं। इनके निबन्धों में विषय की गम्भीरता दृष्टव्य है।
प्रेमचन्द की सभी रचनाओं की भाषा अत्यन्त सहज एवं सरल है। हिन्दी भाषा में उर्दू के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा जगभाषा के निकट की भाषा है। भाषा को अत्यन्त प्रभावशाली बनाने के लिए लोक प्रचलित मुहावरों का सफल प्रयोग देखते ही बनता है।
सच्चे अर्थों में इन्हें जनता का कलाकार, साहित्यकार व लेखक स्वीकार किया गया है। वास्तव में इनकी रचनाओं में समूचे युग का सच्चा चित्र अंकित है। इसी कारण आज भी इनका सम्पूर्ण साहित्य प्रासंगिक है अर्थात् जितना उसका महत्त्व उनके समय में था आज भी है। आज भी इनकी रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ा जाता है। इसलिए मैंने भी हिन्दी के अनेक महान् लेखकों में से इन्हें ही अपना प्रिय लेखक स्वीकार किया है।

33. बेरोजगारी की समस्या
संकेत : भूमिका, जनसंख्या में वृद्धि, अधूरी शिक्षा प्रणाली, उद्योग-धंधों की अवनति, सामाजिक तथा धार्मिक मनोवृत्ति, सरकारी विभागों में छंटनी, जनसंख्या वृद्धि पर रोक और शिक्षा, उद्योग एवं कृषि का विकास, उपसंहार।
आज भारत के सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं; जैसे महँगाई, बेरोज़गारी, आतंकवाद आदि। इन सब में बेरोज़गारी की समस्या प्रमुख है। बेरोज़गारी की समस्या ने परिवारों की आर्थिक दशा को खोखला कर दिया है। आज हम स्वतंत्र अवश्य हैं परंतु हम अभी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हुए हैं। चारों ओर चोरी-डकैती, छीना-झपटी, लूटमार और कत्ल के समाचार सुनाई पड़ते हैं। आज देश में जगह-जगह पर उपद्रव एवं हड़तालें हो रही हैं। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास न जाने कहाँ चले गए हैं। प्रत्येक मानव को अपनी तथा अपने परिवार की रोटियों की चिंता है चाहे उनका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से। निरक्षर तो फिर भी अपना पेट भर लेते हैं परंतु साक्षर वर्ग की आज बुरी हालत है।
बेकारी का चरमोत्कर्ष तो उस समय दिखाई दिया, जब रुड़की विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रशिक्षित इंजीनियरों को उपाधि देने हेतु 1967 के दीक्षांत समारोह में भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ी हुईं, उसी समय लगभग एक हज़ार इंजीनियरों ने खड़े होकर एक स्वर में कहा, ‘हमें भाषण नहीं, नौकरी चाहिए।’ प्रधानमंत्री के पास उस समय कोई उत्तर न था।
हमारे देश में बेकारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
हमारे देश में जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष भर में जितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, उससे कई गुणा अधिक बेकारों की संख्या बढ़ जाती है। अनेक अप्राकृतिक उपायों के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप ही बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है।
हमारी शिक्षा-प्रणाली अधूरी एवं दोषपूर्ण है। परतंत्र भारत में अंग्रेज़ों ने ऐसी शिक्षा-पद्धति केवल क्लर्कों को पैदा करने के लिए ही लागू की थी परंतु अब स्वतंत्र भारत में समयानुसार समस्याएँ भी बदल गई हैं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “प्रतिवर्ष नौ लाख पढ़े-लिखे लोग नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं जबकि हमारे पास नौकरियाँ शतांश के लिए भी नहीं हैं। हमें बी०ए० नहीं चाहिएँ, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ चाहिएँ।” उनका यह कथन हमारी शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत करता है।
प्राचीन काल में हमारे देश के प्रत्येक घर में कोई-न-कोई उद्योग-धंधा चलता था। कहीं चरखा काता जाता था, कहीं खिलौने बनते थे तो कहीं गुड़। इन्हीं उद्योग-धंधों से लोग रोजी-रोटी कमाते थे परंतु अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें नष्ट कर दिया जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसीलिए पढ़े-लिखे लोग भूखों मरना पसंद करते हैं परंतु वे मजदूरी करना पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं कि दुनिया कहेगी कि पढ़-लिखकर मजदूरी कर रहा है। यही मिथ्या स्वाभिमान मनुष्य को कुछ करने नहीं देता। पढ़ाई-लिखाई ने मजदूरी करने को मना तो नहीं किया है।
हमारे समाज की धार्मिक तथा सामाजिक मनोवृत्ति भी बेकारी को बढ़ावा देती है। वर्तमान युग में साधु-संन्यासियों को भिक्षा देना पुण्य समझा जाता है। दानियों की उदारता देखकर बहुत से स्वस्थ व्यक्ति भी भिक्षावृत्ति पर उतर आते हैं। इस प्रकार, बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ सामाजिक नियम कुछ ऐसे हैं कि वर्ण-व्यवस्था के अनुसार विशेष-विशेष वर्गों के लिए विशेष-विशेष कार्य हैं। सरकारी विभागों में भी वर्ण-व्यवस्था के अनुसार काम दिए जाते हैं। यदि उन्हें काम मिले तो करें अन्यथा हाथ-पर-हाथ धरकर बैठे
रहें। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से भी बेरोज़गारी को बढ़ावा मिलता है। बेकारी के कारण युवा-आक्रोश और असंतोष ने समाज में अव्यवस्था एवं अराजकता उत्पन्न कर दी है।
निम्नलिखित उपायों द्वारा बेकारी दूर की जा सकती है-
देश में जनसंख्या वृद्धि को रोककर बेकारी की समस्या को काफी सीमा तक हल किया जा सकता है। बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए विवाह की आयु का नियम कठोरता से लागू करना चाहिए। साथ ही, हमें शिक्षा-पद्धति में सुधार करना होगा। शिक्षा को व्यावहारिक बनाना होगा। विद्यार्थियों में आरंभ से ही स्वावलंबन की भावना पैदा करनी होगी।
सरकार को कुटीर उद्योगों तथा घरेलू दस्तकारी को प्रोत्साहन देना चाहिए; जैसे सूत कातना, कागज़ बनाना, शहद तैयार करना आदि। उद्योग-धंधों एवं धन की उचित व्यवस्था न होने के कारण गाँव के बड़े-बड़े कारीगर भी बेकार हैं। भारतीय किसान कृषि के लिए वर्षा पर आश्रित रहता है। अतः उसे अपने खाली समय में कुटीर उद्योग चलाने चाहिएँ। इससे उसकी तथा देश की आर्थिक दशा सुदृढ़ होगी। आजकल हज़ारों ग्रामीण शहरों में आकर बसते जा रहे हैं, इससे बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है।
केंद्र तथा राज्य सरकारें इस दिशा में व्यापक पग उठा रही हैं। चाहे हमारी सरकार बेकारी पर काबू पाने में अभी सफल नहीं हो सकी है परंतु ऐसा विश्वास किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रोज़गार के साधन जुटाकर बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार विस्तृत पग उठाएगी। अब वह दिन दूर नहीं, जब देश के प्रत्येक नागरिक को काम मिलेगा और देश का भविष्य उज्ज्वल होगा।

34. पर्यावरण संरक्षण
संकेत : भूमिका, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण की समस्या, उपसंहार।
जिस स्थान पर हम रहते हैं, उसके आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। आज के युग में पर्यावरण की शुद्धता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। क्योंकि मनुष्य ने उन्नति की अंधी दौड़ में भाग लेने के चक्र में पड़कर पर्यावरण की शुद्धता को भुला दिया है। इसलिए आज पर्यावरण की रक्षा करना अति अनिवार्य हो गया है। पर्यावरण की शुद्धता मानव के लिए उतनी ही अनिवार्य है, जितना साँस लेना। प्राचीनकाल में मानव का जीवन अत्यंत सरल एवं सहज था। वह प्रकृति के साहचर्य में रहता हुआ प्राकृतिक जीवन जीता था, किंतु आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने अपनी प्राचीन सहचरी प्रकृति को तरह-तरह की हानियाँ पहुँचा दी हैं। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहा।
अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ, शुद्ध एवं पावन कैसे रखें ? इसके लिए हमें फिर प्रकृति की ही शरण में जाना पड़ेगा अर्थात् अधिक-से-अधिक पेड़-पौधे उगाने पड़ेंगे क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इनमें कार्बन-डाइऑक्साइड जैसी जहरीली एवं पर्यावरण विरोधी गैसों का पोषण करने की अत्यधिक क्षमता है और बदले में ऑक्सीजन देने की शक्ति भी। अतः स्पष्ट है कि हम अपने पर्यावरण को पेड़-पौधों की सहायता से सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार नदियों में बहने वाले जल को शुद्ध रखकर भी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।
वायु-प्रदूषण भी पर्यावरण का ही कुरूप है। यदि हम शुद्ध वातावरण में साँस लेना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हमें वायु प्रदूषण को रोकना होगा। इसके लिए फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ व गैसों को कम करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ वाहनों से निकलने वाले धुएँ पर भी नियंत्रण रखना होगा।
पर्यावरण की शुद्धता एवं सुरक्षा के लिए हमें अपने घरों का कूड़ा-कर्कट ढककर रखना पड़ेगा या उसे व्यवस्थित ढंग से नष्ट करना होगा। आज पोलिथिन का प्रयोग भी हमारे पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।
संसार के प्रत्येक नागरिक का यह पावन कर्त्तव्य बनता है कि वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचे अथवा पर्यावरण प्रदूषित हो। हमारा पावन कर्त्तव्य है कि हम अधिक-से-अधिक पेड़-पौधे उगाएँ और पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोकें। यदि हम चाहते हैं कि धरती स्वर्ग-सी बनी रहे, तो इसके लिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध एवं सुरक्षित रखना पड़ेगा।
35. होली
संकेत: भूमिका, इतिहास, कृषि का पर्व, रंगों का त्योहार, कुप्रथा, उपसंहार।
भारत त्योहारों और पर्यों का देश है। यहाँ हर वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। रक्षाबन्धन, दीपावली, दशहरा, होली आदि यहाँ के सुप्रसिद्ध त्योहार हैं। अन्य पर्यों की भान्ति होली भी भारत का प्रमुख पर्व है। यह भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार समाज की एकता, मेल-जोल और प्रेम भावना का प्रतीक माना जाता है।
होली के त्योहार का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इसका सम्बन्ध राजा हिरण्यकश्यप से है। हिरण्यकश्यप निर्दयी और नास्तिक राजा था। वह अपने-आपको भगवान मानता था तथा चाहता था कि प्रजा उसे परमात्मा से भी बढ़कर समझे तथा उसकी पूजा करे। उसके पुत्र एवं ईश्वर-भक्त प्रह्लाद ने उसका विरोध किया। इस पर क्रोधित होकर उसने उसे मार डालने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका थी। उसे वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। लकड़ियों के एक ढेर पर होलिका प्रसाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और फिर लकड़ी के ढेर को आग लगा दी गई। होलिका जलकर राख हो गई पर प्रसाद ज्यों-का-त्यों बैठा रहा। इसलिए लोग इस घटना को याद करके होली मनाते हैं।
होली का त्योहार मनाने का एक और कारण भी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। फरवरी और मार्च के महीने में गेहूँ और चने के दाने अधपके हो जाते हैं। इनको देखकर किसान खुशी से झूम उठता है। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए वह गेहूँ के बालों की अग्नि में आहुति देता है।
होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग रंग, गुलाल, अबीर आदि से त्योहार मनाते हैं। लोग एक-दूसरे पर रंग डालते हैं तथा एक-दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। इस अवसर पर लोगों के चेहरे एवं वस्त्र रंग-बिरंगे हो जाते हैं। चारों ओर मस्ती का वातावरण छा जाता है। वास्तव में यह त्योहार कई दिन पूर्व ही आरम्भ हो जाता है।
यह त्योहार परस्पर भाई-चारे और प्रेम-भाव का त्योहार है। इस अवसर पर कई लोग रात को लकड़ियाँ जलाकर होली की पूजा करते हैं। उसके बाद गाना बजाना करते हैं।
कविवर मैथिलीशरण गुप्त का कथन है-
काली-काली कोयल बोली होली, होली, होली
फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली-पीली चोली।
इस शुभ त्योहार पर कुछ लोग एक-दूसरे पर मिट्टी, कीचड़, पानी आदि फेंकते हैं। यह उचित काम नहीं है। इससे किसी भी पर्व का महत्त्व कम हो जाता है। ऐसा करने से कभी-कभी लड़ाई-झगड़े तक हो जाते हैं तथा वैर भावना जन्म ले लेती है। कुछ लोग इस अवसर पर शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इन सब बुराइयों के कारण ऐसे शुभ त्योहार अपने सच्चे महत्त्व एवं अर्थ को खो बैठते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इस त्योहार को उचित ढंग से मनाएँ तथा हमें उसके महत्त्व को समझने का प्रयास करना चाहिए।
सार रूप में कहा जा सकता है कि होली एक आनन्दमय एवं मस्ती भरा त्योहार है। यह प्रकृति एवं कृषि का त्योहार है। हमें इसकी पवित्रता एवं महत्त्व को समझना चाहिए तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस पर्व पर गोष्ठियों का आयोजन करके हमें समाज में एकता और प्रेम को बढ़ाना चाहिए।

36. दीपावली
संकेत : भूमिका, ऐतिहासिक आधार, दीपावली पर्व की तैयारी, मनाने की विधि, कुप्रथा, उपसंहार।
भारत त्योहारों का देश है। प्रत्येक ऋतु में किसी-न-किसी त्योहार को मनाया जाता है। भारत में फसलों के पकने पर भी त्योहार मनाए जाते हैं। महापुरुषों के जन्मदिन को भी त्योहारों की भान्ति बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भारत के मुख्य त्योहारों-रक्षा बन्धन, दशहरा, दीपावली और होली आदि में दीपावली सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे बड़े जोश एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली का अर्थ है-‘दीपों की पंक्ति’। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की रात बिल्कुल अन्धेरी होती है किंतु भारतीय घर-घर में दीप जलाकर उसे पूर्णिमा से भी अधिक उजियाली बना देते हैं। इस त्योहार का बड़ा महत्त्व है।
इस त्योहार का ऐतिहासिक आधार अति महत्त्वपूर्ण एवं धार्मिक है। इस दिन भगवान् राम लंका-विजय करके अपना वनवास समाप्त करके लक्ष्मण और सीता सहित जब अयोध्या आए तो नगरवासियों ने अति हर्षित होकर उनके स्वागत के लिए रात्रि को नगर में दीपमाला करके अपने आनन्द और प्रसन्नता को प्रकट किया। दीपावली का त्योहार आर्यसमाजी, जैनी और सिक्ख लोग भी विभिन्न रूपों में बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसी दिन आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महासमाधि ली थी और इसी दिन जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसी प्रकार सिक्ख अपने छठे गुरु की याद में इस त्योहार को मनाते हैं जिन्होंने इसी दिन बन्दी गृह से मुक्ति प्राप्त की थी।
इस पर्व की तैयारी घरों की सफाई से आरम्भ होती है जो कि लोग एक-आध मास पूर्व आरम्भ कर देते हैं। लोग शरद् ऋतु के आरम्भ में घरों की लिपाई-पुताई करवाते हैं और कमरों को चित्रों से अलंकृत करते हैं। इससे मक्खी, मच्छर दूर हो जाते हैं। इससे कुछ दिन पूर्व अहोई माता का पूजन किया जाता है। धन त्रयोदशी के दिन लोग पुराने बर्तन बेचते हैं और नए खरीदते हैं। चतुर्दशी को लोग घरों का कूड़ा-करकट बाहर निकालते हैं। लोग कार्तिक मास की अमावस्या को दीपमाला करते हैं।
इस दिन कई लोग अपने इष्ट सम्बन्धियों में मिठाइयाँ बाँटते हैं। बच्चे नए-नए वस्त्र पहनकर बाजार जाते हैं। रात को पटाखे तथा आतिशबाजी चलाते हैं। बहुत-से लोग रात को लक्ष्मी पूजा करते हैं। कई लोगों का विचार है कि इस रात लक्ष्मी अपने श्रद्धालुओं के घर जाती है। इसलिए प्रायः लोग अपने घर के द्वार उस रात बन्द नहीं करते ताकि लक्ष्मी लौट न जाए। व्यापारी लोग वर्षभर के खातों की पड़ताल करते हैं और नई बहियाँ लगाते हैं।
दीपावली के दिन जहाँ लोग शुभ कार्य एवं पूजन करते हैं वहाँ कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। जुआ खेलने वाले लोगों का विश्वास है कि यदि इस दिन जुए में जीत गए तो फिर वर्ष भर जीतते रहेंगे तथा लक्ष्मी की उन पर कृपा बनी रहेगी। कहीं-कहीं पटाखों को लापरवाही से बजाते समय बच्चों के हाथ-पाँव भी जल जाते हैं और कहीं-कहीं पटाखों के कारण आग लगने की दुर्घटना भी होती है। अतः इस पावन पर्व को हमें सदा सावधानी से मनाना चाहिए।
दीपावली का त्योहार मानव जाति के लिए शुभ काम करने की प्रेरणा देने वाला है। जैसे दीपक जल कर अन्धकार को समाप्त करके प्रकाश फैला देता है, वैसे ही दीपावली भी अज्ञानता के अन्धकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में भर देती है। देश और जाति की समृद्धि का प्रतीक यह त्योहार अत्यन्त पावन और मनोरम है।
37. आदर्श विद्यार्थी
संकेत : • भूमिका, ‘विद्यार्थी’ शब्द का अर्थ, प्राचीनकाल में विद्यार्थी जीवन, आदर्श विद्यार्थी के गुण, सादा जीवन और उच्च विचार, संयम और परिश्रम, विद्यार्थी और खेल-कूद, उपसंहार।।
विद्यार्थी काल मानव के भावी जीवन की आधारशिला है। यदि यह आधारशिला मज़बूत है तो उसका जीवन निरंतर विकास करेगा, नहीं तो आने वाले कल की बाधाओं के सामने वह टूट जाएगा। यदि छात्र ने विद्यार्थी जीवन में परिश्रम, अनुशासन, संयम और नियम का अच्छी प्रकार से पालन किया है तो उसका भावी जीवन सुखद होगा। सभ्य नागरिक के लिए जिन गुणों का होना ज़रूरी है, वे गुण तो बाल्यकाल में विद्यार्थी के रूप में ही ग्रहण किए जाते हैं। जिस विद्यार्थी ने मन लगाकर विद्या का अध्ययन किया है; माता-पिता और गुरुजनों की विनम्रतापूर्वक सेवा की है; वह अवश्य ही एक सफल नागरिक बनेगा।
‘विद्यार्थी’ संस्कृत भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों के मेल से बना है-‘विद्या’ और ‘अर्थी’ । इसका अर्थ है-विद्या चाहने वाला। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए ही विद्यालय में जाता है और विद्या से प्रेम करता है। वस्तुतः ‘विद्यार्थी’ शब्द में ही आदर्श विद्यार्थी के सभी गुण निवास करते हैं। अतः जिसके जीवन का लक्ष्य विद्या-प्राप्ति है, जो विद्या का अनुरागी है और जो निरंतर विद्यार्जन में ही अपना समय व्यतीत करता है, वही आदर्श विद्यार्थी है।
हमारे ऋषि-मुनियों ने मानव-जीवन को चार आश्रमों में बाँटा है। वे चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम ही विद्यार्थी जीवन है। उस काल में विद्याध्ययन के लिए बालक घर-परिवार से दूर आश्रम में जाते थे। आश्रम में तपस्या, ब्रह्मचर्य, अनुशासन और गुरु-सेवा करते हुए वे विद्या प्राप्त करते थे। स्वयं भगवान कृष्ण सुदामा के साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। विद्यार्थी काल में जो लोग एकाग्र मन से विद्या का अध्ययन करते रहे हैं, वही आगे चलकर महान बने हैं। अर्जुन, अभिमन्यु, एकलव्य, श्रीकृष्ण आदि के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं।
संसार में गुणों से ही मनुष्य की पूजा होती है। संस्कृत में कहा भी गया है-“गुणैः हि सर्वत्र पदं निधीयते” अर्थात् गुणों द्वारा ही मनुष्य सर्वत्र ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है। विद्यार्जन में ही सारे गुण निवास करते हैं। विद्यार्थी का जीवन साधना की अवस्था है। इस काल में वह ऐसे गुणों को ग्रहण कर सकता है जो आने वाले काल में न केवल उसके लिए अपितु समूचे समाज के लिए उपयोगी हों। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता परम आवश्यक है। यदि विद्यार्थी उदंड और उपद्रवी अथवा कटुभाषी है तो वह कभी भी आदर्श विद्यार्थी नहीं बन सकता। विद्या का लक्ष्य विनय की प्राप्ति है-विद्या ददाति विनयं । एक अच्छे गुरु से विद्या प्राप्त करने के तीन उपाय हैं-नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। अतः एक सच्चे विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए।
अनुशासन का भी विद्यार्थी जीवन में उतना ही महत्त्व है, जितना कि विनम्रता का। जो विद्यार्थी अनुशासनप्रिय हैं, वे ही मेधावी छात्र बनते हैं लेकिन जो विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं, वे अपने देश, अपनी जाति और अपने माता-पिता का अहित करते हैं। अनुशासन का पालन करने से ही विद्यार्थी का सही अर्थों में बौद्धिक विकास होता है।
आदर्श विद्यार्थी का मूल मंत्र है सादा जीवन और उच्च विचार। जो बालक विद्यार्थी काल में सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनका मन विद्या में लगा रहता है लेकिन आजकल पश्चिमी सभ्यता के दुष्प्रभाव के कारण विद्यार्थी फैशनपरस्ती के शिकार बन रहे हैं। माता-पिता भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सादगी के साथ ही उच्च विचार जुड़े हुए हैं। जिस विद्यार्थी का ध्यान बाहरी दिखावे की ओर रहेगा, वह अपने अंदर उच्च विचारों का विकास कैसे कर पाएगा ? इसके साथ-साथ विद्यार्थी को सदाचार और स्वावलंबन का भी पालन करना चाहिए।
एक आदर्श विद्यार्थी के लिए संयम और परिश्रम दोनों ही आवश्यक हैं। विद्यार्थी जीवन संयमित और नियमित होना चाहिए। जीवन में उचित रीति का पालन करने वाले विद्यार्थी कभी असफल नहीं होते। एक आदर्श विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और निरंतर परिश्रम करना एक अच्छे विद्यार्थी के गुण हैं। संयम-नियम का पालन करने से ही विद्यार्थी का मन अध्ययन में लगता है। परिश्रम के बिना विद्या नहीं आती। संस्कृत में कहा भी गया है-
सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम्, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखं ।
सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखं ॥
आज के विद्यार्थी के लिए खेल-कूद में भाग लेना भी अनिवार्य है। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जो विद्यार्थी खेल-कूद में भाग न लेकर केवल किताबी कीड़े बने रहते हैं, वे शीघ्र ही रोगी बन जाते हैं। खेल-कूद में भाग लेने से विद्यार्थी संयम और परिश्रम के नियमों को भी सीखता है। आज के स्कूलों और कॉलेजों में खेलों के लिए समुचित व्यवस्था है। अतः विद्यार्थियों को विद्याध्ययन के साथ-साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए।
इस प्रकार से आज का विद्यार्थी यदि देश का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, अपने माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह करना चाहता है तो उसे वे सब गुण अपनाने होंगे जो उसके विकास के लिए आवश्यक हैं।

38. विद्यार्थी और अनुशासन अथवा अनुशासन का महत्त्व
संकेत : भूमिका, अनुशासन का अर्थ, विद्यार्थी और अनुशासन, प्राचीनकाल में विद्यार्थी जीवन, वर्तमान स्थिति, अनुशासनहीनता के कारण, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, उपसंहार।
किसी भी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। यदि नींव मज़बूत है तो उस पर बना भवन भी सुदृढ़ होगा और लंबे काल तक टिका रहेगा। इसी प्रकार से राष्ट्र की सुदृढ़ता उसके युवकों पर निर्भर करती है। यदि हमारे देश के युवक अनुशासित एवं सुशिक्षित होंगे तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा, विद्यार्थी अनुशासित नहीं होंगे तो कभी भी हमारे देश पर विपत्ति के बादल मंडरा सकते हैं।
‘अनुशासन’ शब्द का अर्थ है-शासन के पीछे-पीछे चलना। शासन का अर्थ है-सुव्यवस्था अर्थात समाज को सुचारु रूप से चलाने के नियमों का पालन करना । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन अनिवार्य है। परिवार हो या समाज, सर्वत्र अनुशासन का पालन करने से मानव जीवन समृद्ध होता है। अनुशासन के अनेक लाभ हैं। इसका पालन करने से आलस्य और कायरता दूर भागते हैं। मनुष्य अपने कर्तव्य का सही पालन करता है। व्यक्ति में सच्चाई और ईमानदारी जैसे सद्गुण विकसित होते हैं।
विद्यार्थी जीवन में अनुशासन नितांत आवश्यक है। विद्यार्थी एक नन्ही कोंपल के समान होता है। उसे जो भी रूप दिया जाए, वह उसे ग्रहण करता है। उसका मन शीघ्र प्रभावित होता है। अतः बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी को अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखें कि बालक-बालिकाएँ अपना-अपना काम नियमित रूप से करें। इस दिशा में माता-पिता का दायित्व और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। बच्चे की शिक्षा का प्रथम विद्यालय उसका घर ही है। यदि माता-पिता स्वयं अनुशासित हैं तो बालक भी अनुशासन की भावना ग्रहण करेगा।
प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। 25 वर्ष तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और यह काल शिक्षा ग्रहण करने में व्यतीत करते थे। उन दिनों गुरुकुलों का वातावरण बहुत ही पावन और अनुशासित होता था। प्रत्येक विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करता था। शिक्षा के साथ-साथ उसे गुरुकुल के सारे काम भी करने पड़ते थे। छोटे-बड़े या
अमीर-गरीब सभी एक ही गुरु के चरणों में विद्या ग्रहण करते थे। श्रीकृष्ण और सुदामा ने इकट्ठे संदीपन ऋषि के आश्रम में अनुशासनबद्ध होकर शिक्षा ग्रहण की।
आज हमारे देश के विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव है। वे न तो माता-पिता का कहना मानते हैं और न ही गुरुजनों का। प्रतिदिन स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें होती रहती हैं। इस प्रकार के समाचार पढ़ने को मिलते रहते हैं कि विद्यार्थियों ने बस जला डाली या पथराव किया। पुलिस और विद्यार्थियों की मुठभेड़ तो होती ही रहती है। राजनीतिक दल भी समय-समय पर अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को भड़काते रहते हैं। विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। ये विद्यार्थी परीक्षाओं में नकल करते हैं, शिक्षकों को धमकाते हैं और विश्वविद्यालयों के वातावरण को दूषित करते रहते हैं। अनेक विद्यार्थी हिंसात्मक कार्रवाई में भी भाग लेने लगे हैं। इससे राज्य की सुख-शांति में बाधा उत्पन्न होती है। निश्चय ही, आज विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी आ चुकी है।
आज की शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध भी विद्यार्थियों को अनुशासनहीन बनाता है। वे विद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी रहती है। भवन छोटे होते हैं और शिक्षकों की संख्या कम। कॉलेजों में तो एक-एक कक्षा में सौ-सौ विद्यार्थी होते हैं। ऐसी अवस्था में क्या तो शिक्षक पढ़ाएगा और क्या विद्यार्थी पढ़ेंगे। कॉलेजों में छात्रों के दैनिक कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। रचनात्मक कार्यों के अभाव में छात्र का ध्यान व्यर्थ की बातों की ओर जाता है। यदि प्रतिदिन विद्यार्थी के अध्ययन-अध्यापन की ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से वह अपना काम अनुशासनपूर्वक करेगा।
छात्रों में अनुशासन की भावना स्थापित करने के लिए यह ज़रूरी है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा के लिए कुछ स्थान हो। इससे विद्यार्थी को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान होगा। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षण के साथ-साथ खेल-कूद को भी अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एन०सी०सी० और एन०एस०एस० जैसे रचनात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
वर्तमान शिक्षण-पद्धति में परिवर्तन करके महापुरुषों की जीवनियों से भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जाना चाहिए। यथासंभव व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि स्कूल से निकलते ही विद्यार्थी अपने व्यवसाय का शीघ्र चयन करें। प्रतिमाह मासिक परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को सुचारु ढंग से चलाने के लिए त्रैमासिक और अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ भी आयोजित की जाएँ। सबसे बढ़कर विभिन्न राजनीतिक दलों को शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार भी यह बात पूरी तरह से जान ले कि छात्रों में अनुशासन स्थापित किए बिना देश सुदृढ़ नहीं हो सकता।
39. पुस्तकालय का महत्व
सकेत : भूमिका, पुस्तकालय का महत्त्व, पुस्तकालय के प्रकार, पुस्तकालय का लक्ष्य, विश्व के पुस्तकालय, पुस्तकालय के लाभ, उपसंहार।
‘पुस्तकालय’ शब्द पुस्तक + आलय दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है-वह स्थान या घर जहाँ पर काफी मात्रा में पुस्तकें रखी जाती हैं। आज के युग में पुस्तकें हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह प्रत्येक पुस्तक को खरीद सके। आजकल पुस्तकें बहुत महँगी हो चुकी हैं। अतः हमें पुस्तकालयों की शरण लेनी पड़ती है।
छोटे-छोटे स्कूलों से लेकर बड़े-बड़े स्कूल और कॉलेज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए गए हैं परंतु ज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल है कि ये शिक्षण-संस्थाएँ एक निश्चित सीमा और निश्चित ज्ञान में पूर्ण रूप से ज्ञान-साक्षात्कार नहीं करा सकतीं। इसलिए ज्ञान-पिपासुओं को पुस्तकालय का सहारा लेना पड़ता है। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थीं जिनमें एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था परंतु आज के मशीनी युग में भी जबकि पुस्तकों का मूल्य प्राचीन काल की अपेक्षा बहुत ही कम है, एक व्यक्ति अपनी ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के लिए सभी पुस्तकें खरीदने में असमर्थ है। पुस्तकालय हमारी इस असमर्थता में बहुत सहायक हैं।
पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के होते हैं। कई विद्या-प्रेमी, जिन पर लक्ष्मी की कृपा होती है, अपने उपयोग के लिए अपने घर में ही पुस्तकालय की स्थापना करते हैं। ऐसे पुस्तकालय ‘व्यक्तिगत पुस्तकालय’ कहलाते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता की दृष्टि से इनका महत्त्व कम होता है। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय कॉलेजों और विद्यालयों में होते हैं। इनमें बहुधा उन्हीं पुस्तकों का संग्रह होता है जो पाठ्य विषयों से संबंधित होती हैं। इस प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक उपयोग में भी नहीं आते। इनका उपयोग छात्र और अध्यापक ही करते हैं परंतु ज्ञानार्जन और शिक्षा की पूर्णता में इनका सर्वाधिक महत्त्व है। ये पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होते। इनके बिना शिक्षालयों की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
तीसरे प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में देश-विदेश में छपी विभिन्न विषयों की पुस्तकों का विशाल संग्रह होता है। इनका उपयोग भी बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा होता है। चौथे प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा होता है। आजकल ग्रामों में भी ग्राम पंचायतों के द्वारा सबके उपयोग के लिए पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं होता। आजकल एक अन्य प्रकार के पुस्तकालय दिखाई देते हैं, उन्हें ‘चल-पुस्तकालय’ कहते हैं। ये मोटरों या गाड़ियों में बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करना होता है। इनमें अधिकतर प्रचार-साहित्य ही होता है।
पुस्तकालय का कार्य पाठकों के उपयोग के लिए सभी प्रकार की पुस्तकों का संग्रह करना है। अपने पाठकों की रुचि और आवश्यकता को देखते हुए पुस्तकालय अधिकारी देश-विदेश में मुद्रित पुस्तकें प्राप्त करने में सुविधा के लिए पुस्तकों की एक सूची तैयार करते हैं। पाठकों को पुस्तकें प्राप्त कराने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। पुस्तकालय में पाठकों के बैठने और पढ़ने के लिए समुचित व्यवस्था होती है। पढ़ने के स्थान को ‘वाचनालय’ कहते हैं। पाठकों को घर पर पढ़ने के लिए भी पुस्तकें दी जाती हैं परंतु इसके लिए एक निश्चित राशि देकर पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। पुस्तकालय में विभिन्न पत्रिकाएँ भी होती हैं।
पुस्तकालयों की दृष्टि से रूस, अमेरिका और इंग्लैंड सबसे बड़े देश हैं। मॉस्को के लेनिन पुस्तकालय में लगभग डेढ़ करोड़ मुद्रित पुस्तकें संगृहीत हैं। वाशिंग्टन (अमेरिका) के काँग्रेस पुस्तकालय में चार करोड़ से भी अधिक पुस्तकें हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय समझा जाता है। इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में पचास लाख पुस्तकों का संग्रह है। भारत में कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में दस लाख पुस्तकें हैं। केंद्रीय पुस्तकालय, बड़ोदरा में लगभग डेढ़ लाख पुस्तकों का संग्रह है। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला में बहुत बड़े पुस्तकालय थे।
पुस्तकालय के अनेक लाभ हैं। ज्ञान-पिपासा की शांति के लिए पुस्तकालय के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी का केवल पथ-प्रदर्शन करता है। ज्ञानार्जन की क्रिया पुस्तकालय से ही पूरी होती है। देश-विदेश के तथा भूत और वर्तमान के विद्वानों के विचारों से अवगत कराने में पुस्तकालय हमारा सबसे बड़ा साथी है। आर्थिक दृष्टि से भी पुस्तकालय का महत्त्व कम नहीं है। एक व्यक्ति जितनी पुस्तकें पढ़ना चाहता है, उतनी खरीद नहीं सकता। पुस्तकालय उसकी इस कमी को भी पूरी कर देता है। कहानी, उपन्यास, कविता और मनोरंजन विषयों की पुस्तकें भी वहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। अवकाश के समय का सदुपयोग पुस्तकालय में बैठकर किया जा सकता है। अतः आधुनिक युग में शिक्षित व्यक्ति के जीवन में पुस्तकालय का काफी महत्त्व है।
दूरदर्शन तथा फिल्मों ने पुस्तकों के प्रकाशन को अत्यधिक प्रभावित किया है लेकिन पुस्तकों की उपयोगिता प्रत्येक युगं में बनी रहेगी। सामान्य पाठक पुस्तकों को खरीद नहीं सकता। अतः उसे पुस्तकालय का ही सहारा लेना पड़ता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की अत्यधिक आवश्यकता है। अनपढ़ता को दूर करने में पुस्तकालयों का बड़ा योगदान हो सकता है।

40. आदर्श अध्यापक
संकेत : भूमिका, जीवन लक्ष्य का चुनाव अनिवार्य, मेरा जीवन लक्ष्य अध्यापक बनना, अध्यापन एक महान कार्य, आदर्श अध्यापक सच्चा सेवक, विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना शिक्षक का कर्तव्य, उपसंहार।
मानव-जीवन एक यात्रा के समान है। यदि यात्री को यह ज्ञात हो कि उसे कहाँ जाना है तो वह अपनी दिशा की ओर अग्रसर होना शुरु हो जाता है किंतु यदि उसे अपने गंतव्य का ज्ञान नहीं होता तो उसकी यात्रा निरर्थक हो जाती है। इसी प्रकार, यदि एक विद्यार्थी को ज्ञान हो कि उसे क्या करना है तो वह उसी दिशा में प्रयत्न करना आरंभ कर देगा और सफलता भी प्राप्त करेगा। इसके विपरीत, उद्देश्यहीन अध्ययन उसे कहीं नहीं ले जाता।
ऊपर बताया गया है कि जीवन एक यात्रा के समान है। मैं भी जीवन रूपी चौराहे पर खड़ा हूँ। यहाँ से कई मार्ग अलग-अलग दिशाओं को जा रहे हैं। मेरे समक्ष अनेक सपने हैं और लोगों के अनेक सुझाव भी हैं। कोई कहता है कि अध्योपक का कार्य सर्वोत्तम है क्योंकि अध्यापक राष्ट्र-निर्माता है। कोई कहता है कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करो। कोई कहता है, नहीं, इंजीनियर बनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कभी-कभी मन में यह भी आता है कि एक सफल व्यापारी बनूँ। फिर सोचता हूँ कि व्यापार में ईमानदारी नहीं। मेरे कुछ साथी भी हैं, वे भी अपने मन में कुछ सपने पाल रहे हैं। कोई डॉक्टर बनकर अधिकाधिक रुपया कमाना चाहता है तो कोई उद्योगपति बनना चाहता है। कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति में प्रवेश करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कोई अभिनेता बनना चाहता है तो कोई लेखक बनकर यश प्राप्त करना चाहता है।
जीवन में लक्ष्य का चुनाव अपनी इच्छाओं एवं अपने साधनों के अनुरूप करना चाहिए। ध्येय चुनतें समय स्वार्थ और परमार्थ में समन्वय रखना चाहिए। अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति को भी सामने रखना चाहिए। दूसरों का अंधानुकरण करना उपयुक्त नहीं। मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है। मैं एक आदर्श शिक्षक बनना चाहता हूँ। भले ही लोग इसे एक सामान्य लक्ष्य कहें परंतु मेरे लिए यह एक महान लक्ष्य है जिसकी पूर्ति के लिए मैं भगवान से नित्य प्रार्थना करता हूँ। अध्यापक बनकर भारत का भार उठाने वाले भावी नागरिक तैयार करना मेरी महत्वाकांक्षा है।
आज की शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों को देखकर मेरा मन निराश हो जाता है। आज शिक्षक शिक्षा का सच्चा मूल्य नहीं समझते। वे शिक्षा को एक व्यवसाय समझने लग गए हैं। धन कमाना ही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया है। बड़े-बड़े पूँजीपति पब्लिक स्कूलों में इसलिए धन लगा रहे हैं ताकि रुपया कमा सकें। वे यह भूल गए हैं कि अध्यापन पावन एवं महान कार्य है। शिक्षक ही राष्ट्र की भावी उन्नति का जीवन बनाते, सुधारते और सँवारते हैं। इस संसार से अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का दीपक जलाते हैं। छात्र-छात्राओं को नाना प्रकार की विद्याएँ देकर उन्हें विद्वान एवं योग्य नागरिक बनाते हैं। शिक्षक ही निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। थोड़े धन से संतुष्ट रहकर वे आने वाली पीढ़ी को तैयार करते हैं और उनमें उत्तम गुणों का विकास करते हैं। आज हमारे देश में जो भ्रष्टाचार एवं मूल्यों की गिरावट आ चुकी है, उसके लिए बहुत कुछ हमारे शिक्षक तथा शिक्षा-व्यवस्था दोषी है।
प्राचीनकाल में हमारे गुरुकुलों में सच्चे अर्थों में शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए गुरुकुल में रहना अनिवार्य होता था। शिक्षक भी गुरुकुल में ही रहता था। उसका समूचा जीवन अपने विद्यार्थियों के लिए होता था। यही कारण था कि बड़े-बड़े राजा भी अपने पुत्रों को वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। शिक्षक अपने जीवन के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान देता था। आदर्श शिक्षक समाज का सच्चा सेवक होता है। उसके सामने राष्ट्र-सेवा का आदर्श होता है। मैं ऐसा ही शिक्षक बनकर विद्यार्थियों को स्वावलंबन, सेवा, सादगी, स्वाभिमान, अनुशासन और प्रामाणिकता का पाठ पढ़ाऊंगा।
आज का विद्यार्थी विद्या को बोझ समझकर उससे दूर भागता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में विद्यार्थी स्कूल जाना बंद कर देते हैं और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करूँगा और यह प्रयास करूँगा कि जो विद्यार्थी स्कूल में आ गया है, वह स्कूल छोड़कर न जाए और अपनी शिक्षा को पूरा करे। छात्रों में अकसर अनुशासनहीनता देखी जा सकती है। उधर कुछ विद्यार्थी राजनीति में भाग लेकर अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके लिए अध्यापक ही दोषी हैं। यदि अध्यापक सही ढंग से पढ़ाएँ तो विद्यार्थी का मन अन्यत्र कहीं नहीं लगेगा। मैं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि विद्यार्थी अपना मन पढ़ाई में लगाएँ और एक अनुशासनबद्ध व्यक्ति की तरह जीवनयापन करें।
मैं अपनी कक्षा को परिवार के समान समयूँगा। अनुशासन का पूरा ध्यान रखूगा। पढ़ाई में कमजोर छात्रों का विशेष ध्यान रलूँगा। उनको अतिरिक्त समय देकर भी पढ़ाऊँगा। मैं मनोविज्ञान के आधार पर अध्यापन करूँगा ताकि विद्यार्थियों की कमजोरी का सही कारण जान सकँ। होनहार छात्रों को भी मैं विशेष रूप से.प्रोत्साहित करूँगा ताकि वे आगे चलकर जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकें। शिक्षा और खेलकूद का उचित समन्वय स्थापित करूँगा। अभिनय, वाद-विवाद, सामान्य ज्ञान तथा निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा अपने विद्यार्थियों को दूंगा। मैं स्वयं सादा रहूँगा और अपनी सादगी, सरलता, विनम्रता तथा सहृदयता से विद्यार्थियों को भी प्रभावित करूँगा। सक्षेप में, मैं एक आदर्श अध्यापक बनने का प्रयास करूँगा क्योंकि एक आदर्श एवं चरित्रवान अध्यापक ही विद्यार्थियों को सही दिशा दे सकता है। ईश्वर करे मेरा उद्देश्य पूर्ण हो और मैं अपने देश की सेवा करूँ।।
41. दूरदर्शन और युवा पीढ़ी
अथवा
दूरदर्शन के लाभ और हानि
संकेत : भूमिका, दूरदर्शन का अर्थ, युवाओं के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग, शिक्षा का सशक्त माध्यम, कुप्रभाव।
आज की भाग-दौड़ की जिंदगी में मनुष्य दिन-भर काम करके शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस करता है। इस थकावट को दूर करने के लिए वह कुछ नवीनता और कौतुहलता चाहता है। शरीर की थकावट को आराम करके दूर किया जा सकता है, परंतु मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद प्रदान करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। समय की कमी के कारण मनुष्य को ऐसे मनोरंजन के साधन की जरूरत होती है, जो घर बैठे ही उसका मनोरंजन कर सके। विज्ञान ने टेलीविज़न का आविष्कार करके एक ऐसा जादू उपलब्ध करवा दिया है, जो मनुष्य के इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।
टेलीविजन का हिंदी पर्याय ‘दरदर्शन’ है। टेली का अर्थ है-‘दर’ तथा विज़न का अर्थ है-‘दर्शन’ अर्थात् दूर के दृश्यों का आँखों के सामने उपस्थित होना। यह रेडियो तकनीक का ही विकसित रूप है, जिसका आविष्कार श्री जे०एल० बेयर्ड ने 1926 में किया था। टेलीविज़न मनोरंजन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। इसने समाज के प्रत्येक वर्ग-बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सबको प्रभावित किया है। हर परिवार का यह एक आवश्यक अंग बन गया है। यह मनोरंजन का सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। पूरे विश्व के समाचार, नई जानकारियाँ आदि घर बैठे प्राप्त की जा सकती हैं। दूरदर्शन ने आज की युवा पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित किया है।
दूरदर्शन आज की युवा पीढ़ी के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण तथा अति आवश्यक अंग है। यदि युवक इसका नियंत्रित तथा संयमित प्रयोग करते हैं तो टेलीविजन उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, अन्यथा उसके दुष्परिणामों से युवकों को बचाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार एक कुएँ से पानी प्राप्त कर मनुष्य अपनी प्यास बुझा जा सकता है, परंतु यदि वह उसमें कूदकर आत्महत्या कर लें, तो कुएँ का क्या दोष? इसी प्रकार दूरदर्शन युवा पीढ़ी को आधुनिकतम शिक्षा तथा विश्व की प्रत्येक जानकारी देने का साधन है, परंतु यदि आज का युवा छात्र अपना अमूल्य समय बेकार के कार्यक्रम देखकर गंवा देगा, तो हम दूरदर्शन को दोष नहीं दे सकते।
दूरदर्शन शिक्षा का सशक्त माध्यम है। इस पर न केवल औपचारिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा का प्रसारण भी होता है। केवल ध्वनि तथा शब्दों का सहारा लेकर पाठ्यक्रम नीरस हो जाता है। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठों का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन पर जीती-जागती तस्वीर देखकर विद्यार्थियों की अपने पाठ्यक्रम के प्रति रुचि बढ़ जाती है तथा भली-भाँति समझ आ जाती है। इसमें अनपढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए पाठों का प्रसारण किया जाता है।
शैक्षिक सामग्री के अतिरिक्त इससे युवा किसानों को कृषि के आधुनिक यंत्रों, कीटनाशकों तथा नई फसलों की जानकारी मिलती है। दूरदर्शन पर ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनसे प्रेरित होकर आज की युवा पीढ़ी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकती है। विद्यार्थी विश्व की नवीनतम जानकारी तथा देश-विदेश के समाचार प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय इतिहास, सभ्यता तथा संस्कृति पर आधारित अनेक कार्यक्रमों से आज का युवा वर्ग प्राचीन भारतीय गौरव की जानकारी ले सकता है। इस प्रकार दूरदर्शन ने हमारी युवा पीढी के जीवन के प्रत्येक पहल को प्रभावित किया है।
यदि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो दूरदर्शन आज के छात्रों के लिए उपयोगी तथा सहायक कम और बाधक अधिक सिद्ध हुआ है। अधिकतर छात्र ऐसे कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं जिनका संबंध शिक्षा से न होकर मनोरंजन से अधिक हो, जो रोचक व रसीले हों जैसे-फिल्में, गाने, सीरियल, खेल तथा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रमों में हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, छल, फरेब, झूठ, चोरी, बेईमानी के नए ढंग बताए जाते हैं। इन सबका व्यापक प्रभाव हमारे युवा वर्ग पर पड़ रहा है। समाज में चोरी, डकैती, हिंसा तथा भ्रष्टाचार इसी का परिणाम है। केबल पर प्रसारित कार्यक्रमों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए अश्लीलता तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को देखकर आज की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। इस पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है।
ऊपर दिए गए तर्क दूरदर्शन के विरोध में नही हैं, बल्कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों पर हैं, जो छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दूरदर्शन को नकारने से तो उससे प्राप्त सभी लाभ समाप्त हो जाएँगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी संयम में रहकर केवल ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखें। दूरदर्शन तो ऐसा साधन है, जिसका उचित उपयोग करके हम अपना जीवन, समाज तथा देश का भविष्य सुखद, आनंददायक तथा उज्ज्वल बना सकते हैं।

42. मेरा सर्वप्रिय ग्रन्थ-रामचरितमानस/मेरी प्रिय पुस्तक
भूमिका-आज प्रतिदिन सैकड़ों नई-नई पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग भाषाओं में नई-नई पुस्तकें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं तो हिन्दी साहित्य का ही नियमित पाठक हूँ। हिन्दी की अच्छी-अच्छी रचनाएं पढ़ने में मेरी रुचि रही है। हिन्दी का साहित्य उन साहित्यकारों द्वारा लिखा गया है जो स्वयं अभावग्रस्त रहे परन्तु पाठकों के लिए सुन्दर भाव अपनी रचनाओं में छोड़ गए हैं। कुछ रचनाएं मुझे काफी रोचक लगी हैं, परन्तु जिस महान् रचना ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है- वह है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ‘रामचरितमानस’ । यह ग्रन्थ सभ्यता एवं संस्कृति का महान् स्मारक है। यही मेरी प्रिय पुस्तक है।
1. रामचरितमानस पूज्य ग्रन्थ :
गोस्वामी तुलसीदास ने ‘कवितावली’, ‘दोहावली’, ‘विनय-पत्रिका’, ‘कृष्ण गीतावली’, ‘पार्वती मंगल’, ‘जानकी मंगल’ आदि असंख्य रचनाएं लिखी हैं। लेकिन रामचरितमानस उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य है। यह एक महाकाव्य है। इसे ‘मानस’ के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर लोग इसे रामायण भी कहते हैं। जिस प्रकार ईसाइयों में ‘बाईबल’, मुसलमानों में ‘कुरान शरीफ’ तथा सिक्खों में ‘गुरु ग्रन्थ साहिब’ पूज्य ग्रन्थ हैं, उसी प्रकार हिन्दुओं में ‘रामचरितमानस’ पूज्य है। झोंपड़ी से महलों तक यह ग्रन्थ मान्य एवं पूज्य है। प्रत्येक हिन्दू मन्दिर और यहाँ तक कि परिवार में इसकी एक प्रति अवश्य मिलती है। इसकी लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ रही है। संसार की शायद ही कोई भाषा हो जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो। हिन्दी साहित्य में यही वह रचना है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं।
2. श्रेष्ठ महाकाव्य :
इस महाकाव्य में कुल सात काण्ड (अध्याय) हैं। इसका रचनाकाल तुलसीदास ने संवत् 1631 दिया है। यह ग्रन्थ दोहा चौपाई में लिखा गया है। इसकी भाषा साहित्यिक अवधी है। ‘मानस’ के कथानक का आधार वाल्मीकि रामायण है परन्तु इसमें कथा-विस्तार, दार्शनिक विचारों तथा युक्ति भावना के लिए अध्यात्म रामायण, गीता, उपनिषद्, पुराण आदि का भी कवि ने आश्रय लिया है। तुलसी के राम वाल्मीकि के राम न होकर नारायण रूप हैं। अतः मानव में तुलसीदास कवि होने के साथ-साथ व्यक्ति भी हैं परन्तु मुझे तो गोस्वामी के कवि रूप ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। महाकाव्य की जो विशेषताएं हो सकती हैं, वे सब इस रचना में हैं। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय ग्रन्थ संसार की किसी भी महान् रचना का मुकाबला कर सकता है।
3. जीवनोपयोगी कथानक:
‘रामचरितमानस’ में मुझे सबसे प्रिय लगती है उसकी कथावस्तु, जिसमें स्थान-स्थान पर तुलसीदास के सहज नाटकीय-रचना-कौशल और अद्भुत सूझबूझ के दर्शन होते हैं। ‘मानस’ की संवाद शैली अत्युत्तम है। ‘मानस’ का आरम्भ भी संवादों से होता है, मध्य भी संवादों और अन्त भी संवादों से। कथा के आधारभूत तीन संवाद हैं-उमा-शम्भु-संवाद, गरुड़-काकभुषुण्डि-संवाद, अंगद-रावण-संवाद, रावण-मन्दोदरी-संवाद आदि। संवादों के माध्यम से ‘मानस’ की कथा अत्यन्त रोचक, ज्ञानवर्द्धक एवं जीवनोपयोगी बन गई है। मार्मिक स्थलों के चयन में तुलसी जी की दृष्टि बड़ी पैनी है। राम-वनवास, भरत-मिलाप, सीता-हरण, शबरी-प्रसंग, लक्ष्मण-मूर्छा आदि इसी प्रकार के अत्यन्त मार्मिक प्रसंग हैं।
4. आदर्श जीवन :
मूल्य सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में ‘मानस’ की महत्ता इसलिए है कि उसमें पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्शों की स्थापना की गई है। रामकथा में हमारी प्रत्येक परिस्थिति का समावेश है और हमारी समस्याओं का समाधान है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता-पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति तथा पत्नी का पति के प्रति क्या कर्त्तव्य है, आदि की झलक मानस में सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है। दूसरी ओर विद्वान् दार्शनिक और आलोचक ‘मानस’ को ज्ञान का भण्डार बतलाते हैं। तुलसी की यह उक्ति उनकी वाणी पर लागू होती है-
कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि हम सब कह हित होई।
5. भाव एवं कला का सुन्दर समन्वय-मानस भाव-पक्ष और कला-पक्ष दोनों दृष्टियों से उदात्त और भव्य काव्य है। ‘कविता करके तुलसी न लसै कविता लसि पा तुलसी की कला’, इसमें कवि ने स्थान-स्थान पर रचना कौशल का परिचय दिया है। मानस धर्म और साहित्य का पवित्र संगम है। यह समस्त भारतीय दर्शन का सार है। यह नाना पुराण निगमागम सम्मत रचना है। स्वयं कवि ने लिखा है-‘स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा।’ वस्तुतः कवि गोस्वामी ने वेदों, पुराणों और अन्य शस्त्रों का सार ग्रहण करके ‘रामचरितमानस’ के रूप में एक ऐसी संजीवनी तैयार की है जिसका पान कर मानव धन्य हो उठता है।
मानस की भाषा अवधी है। बल्कि इसे साहित्यिक अवधी कहना अधिक उचित होगा। तुलसी की भाषा पात्रानुकूल, सहज, सरल और प्रवाहमयी है। दोहा-चौपाई में लिखा गया यह महाकाव्य साधारण से साधारण पाठक के लिए भी बोधगम्य है। इसमें अलंकारों की छटा भी दर्शनीय है। अलंकारों में रमणीयता के साथ-साथ स्वाभाविकता भी है। कवि ने अर्थालंकारों के साथ-साथ शब्दालंकारों का भी सुन्दर प्रयोग किया है। अस्तु, मुझे यह ग्रन्थ सर्वाधिक प्रिय है। मैं समय-समय पर इसका पाठ करता हूँ। निःसन्देह यह संसार का एक महान् गौरव ग्रन्थ है।

43. मानव और विज्ञान
अथवा
विज्ञान वरदान या अभिशाप
संकेत : भूमिका, विज्ञान और आधुनिक जीवन, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान के चमत्कार, चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार।
आज का युग विज्ञान के चमत्कारों का युग है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है-वि+ज्ञान अर्थात् किसी वस्तु का विशेष ज्ञान। आज विज्ञान की उन्नति ने संसार को चकित कर दिया है। विज्ञान विवेक का द्वार है। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मानव विज्ञान की शरण में आया और विज्ञान मानव के लिए कल्पवृक्ष सिद्ध हुआ। विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों को देखकर मनुष्य दाँतों तले उँगली दबा लेता है। विज्ञान की चकाचौंध देखकर मनुष्य स्तब्ध रह जाता है।
विज्ञान और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखमय बना दिया है। एक विद्वान के अनुसार, “विज्ञान ने अंधों को आँखें दी हैं तथा बहरों को सुनने की शक्ति। उसने जीवन को दीर्घ बना दिया है तथा भय को कम कर दिया है। पागलपन को वश में कर लिया है और रोगों को रौंद डाला है।” मानव ने जहाँ विज्ञान द्वारा इतने सुख प्राप्त किए हैं, वहाँ दुःख भी प्राप्त किए हैं। विज्ञान मानव के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी।
विज्ञान ने मानव को अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में विज्ञान का योगदान है। विज्ञान ने आज मानव की कल्पनाओं को यथार्थ रूप में बदल दिया है। भाप, बिजली और अणुशक्ति को वश में करके विज्ञान ने मानव जीवन को चार चाँद लगा दिए हैं। रॉकेट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसे यंत्रों ने मानव जीवन को ऐश्वर्य की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है।
विज्ञान ने मानव के मनोरंजन के लिए भी अनेक साधन पैदा किए हैं। रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, टेपरिकॉर्डर, सिनेमा आदि से मानव जीवन अधिक रोचक बन गया है। आज हम घर बैठे देश-विदेश के समाचारों को सुन सकते हैं। विदेश में हो रहे कार्यक्रमों को भी घर बैठकर आराम से देख सकते हैं। सिनेमा को जहाँ मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ सिनेमा को शिक्षा के साधन के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य का जीवन सुविधापूर्ण तथा आनंदमय बना दिया है। मशीनों द्वारा ही सब काम संपन्न किए जा सकते हैं। अन्न उगाने तथा वस्त्र बनाने के लिए भी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। पहले लोग मिट्टी के दीपक जलाकर घर में रोशनी करते थे, परंतु आज बटन दबाते ही सारा घर जगमग करने लगता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। एक्स-रे द्वारा शरीर के अंदर के चित्र लिए जाते हैं तथा बीमारियों का पता लगाया जाता है जिससे फेफड़े, दिल, गुर्दे आदि के ऑपरेशन किए जाते हैं। अंधों को दूसरों की आँखें देकर देखने योग्य बनाया जा सकता है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए कोबाल्ट किरणों का आविष्कार किया गया है।
परंतु जब मनुष्य विज्ञान का दुरुपयोग करने लगता है तो वही विज्ञान मानव के लिए अभिशाप बन जाता है। विज्ञान की भयानकता को देखकर मनुष्य का सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग मानव हित के लिए उतना नहीं हुआ, जितना अहित के लिए। विज्ञान ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे विनाशकारी अस्त्र-शस्त्र बनाए हैं जिनसे सारा संसार क्षण भर में नष्ट हो सकता है। द्वितीय महायुद्ध में जितना विनाश हुआ, उसकी पूर्ति शायद विज्ञान सौ वर्षों में भी नहीं कर सकता। हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर गिरे अणु बमों के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। बम के प्रभाव के कारण वहाँ की संतानें अब तक अपंग पैदा होती हैं। तीसरे महायुद्ध की कल्पना करने मात्र से ही हृदय काँप उठता है।
प्रदूषण की समस्या का मूल कारण भी विज्ञान ही है। हवाई जहाजों से बमों की वर्षा करके निरीह जनता तथा उनके घर-बार तबाह किए जाते हैं। विज्ञान से सबसे बड़ी हानि यह है कि इसने मनुष्य को बेकार बना दिया है। मशीनी युग के कारण अनेक लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की नैतिक धारणाएँ शिथिल हो गई हैं। हस्तकलाओं तथा लघु उद्योगों में निपुण अनेक लोग मशीनों की प्रगति के कारण बेकार हो गए हैं। विज्ञान ने मनुष्य को शक्ति दी है, शांति नहीं; सुविधाएँ दी हैं, सुख नहीं।
विज्ञान तो केवल एक शक्ति है। मनुष्य इसका सदुपयोग भी कर सकता है तथा दुरुपयोग भी। वास्तव में, विज्ञान द्वारा जो विनाश हुआ है, उसे विज्ञान पर नहीं थोपा जा सकता क्योंकि वह तो निर्जीव है। उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना तो मनुष्य पर निर्भर करता है। विज्ञान तो मनुष्य का दास है। मनुष्य उसे जैसी आज्ञा देगा, वह वैसा ही करेगा। विज्ञान की स्थिति एक तलवार की भाँति है जिससे किसी के प्राणों की रक्षा भी की जा सकती है तथा किसी के प्राण भी लिए जा सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह विज्ञान का प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए ही करे, विनाश के लिए नहीं।

44. मानव और कंप्यूटर
अथवा
कंप्यूटर : आज की आवश्यकता
संकेत : भूमिका, कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर का कार्य, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग, आर्थिक विकास के लिए लाभकारी, कंप्यूटर मानव प्रगति में सहायक, उपसंहार।
आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने अपने अद्भुत चमत्कारों द्वारा क्रांति उत्पन्न कर दी है। विज्ञान की उन्नति ने मानव को विस्मित कर दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे-ऐसे आविष्कार हो चुके हैं कि मनुष्य उन्हें देखकर दाँतों तले अंगुली दबा लेता है। उनकी चकाचौंध देखकर आज का मानव स्तब्ध रह जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार वैज्ञानिक चमत्कारों में एक ऐसा ही चमत्कार है जिसने मानव के जीवन को सरल एवं सुखद बना दिया है।
गणनाओं की जटिलता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि क्यों न गणनाओं के लिए मशीन का आविष्कार किया जाए? मशीन द्वारा गणना कर सकने की युक्ति आज से लगभग 350 वर्ष पुरानी है। सन 1662 में फ्रांस के एक गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने सर्वप्रथम जोड़ करने की एक मशीन बनाई। इंग्लैंड के निवासी चार्ल्स बावेज ने सन 1833 में मशीन का आविष्कार किया और वह आजीवन उस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का रूप देने का प्रयास करता रहा परंतु सफल न हो सका। आधुनिक कंप्यूटर बनाने का श्रेय विद्युत अभियंता पी० इकरैट, भौतिकशास्त्री जॉहन, डब्ल्यू० मैकली तथा गणितज्ञ जी०वी० न्यूमैन को है। इन तीनों ने पारस्परिक सहयोग द्वारा सन 1944 में एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीमेटर एंड कंप्यूटर रखा गया। वर्ष 1952 में इस मशीन का सुधरा हुआ रूप बाज़ार में आया। इलेक्ट्रॉनिकी की प्रगति के फलस्वरूप एक के बाद एक अधिक कार्यक्षमता वाले कंप्यूटर बनने लगे। तत्पश्चात इनके आकार पर भी नियंत्रण किया गया।
कंप्यूटर वस्तुतः ऐसी मशीन है जो जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने जैसी क्रियाओं को बड़ी शीघ्रता से और शुद्धता के साथ करती है। तदर्थ कंप्यूटर में कार्य निर्देश और आँकड़े भरे जाते हैं। दिए गए (भरे गए) कार्य-निर्देश इस प्रकार के होते हैं जैसे कि किसमें क्या जोड़ना है? घटाना है या भाग करना है ? क्या पढ़ना है, क्या लिखना है ? आदि। कार्य-निर्देशों का क्रमबद्ध संकलन कार्यक्रम कहलाता है। कंप्यूटर सर्वप्रथम इन निर्देशों को पढ़ता है और अपनी स्मृति में बिठा लेता है। पुनः वह कार्यक्रम के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर की सफलता इसी में है कि वह साधारण निर्देशों को एक उचित क्रम से देने पर बड़ी-से-बड़ी जटिल गणना को भी बिना किसी अशुद्धि के शीघ्रता से कर सकता है।
कंप्यूटर ने मानव-जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर संबंधी शिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कंप्यूटर के कोर्स चल रहे हैं। हाल ही में बी०एस०सी० के पश्चात एम०सी०ए० और एम०एस०सी० पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित देशों में कंप्यूटर की आधुनिकतम शिक्षण व्यवस्था है। यह शिक्षण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो प्रकार का है। कंप्यूटर की विभिन्न भाषाएँ हैं, यथाडॉस, लोटस, कोबोल, पासकल, बेसिक आदि।
हमारे आर्थिक, वैज्ञानिक, कला, युद्ध, ज्योतिष, चिकित्सा, मौसम, इंजीनियरिंग आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आर्थिक जीवन में तो इसने क्रांति ही उत्पन्न कर दी है। बैंकों तथा विभिन्न फर्मों के खातों के संचालन और हिसाबकिताब में इसका खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। अनेक राष्ट्रीय बैंकों द्वारा चुंबकीय संख्या वाली चैक-बुक प्रसारित की गई हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में तो इसकी उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बड़े-बड़े उद्योग प्रायः अपना सारा काम कंप्यूटरों द्वारा करने लगे हैं। टी०वी०, रेडियो, वी०सी०आर०, बिजली की मोटरें तथा अन्य इलैक्ट्रीकल वस्तुओं के उत्पादन में कंप्यूटर का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। बड़े-बड़े कारखानों में मशीनों को चलाने में कंप्यूटरों की सहायता ली जा रही है। अब रोबोट (लौह पुरुष) कंप्यूटरों की सहायता से ऐसी मशीनों को चला सकते हैं जिनका संचालन मानव के लिए कठिन है। युद्ध के क्षेत्र में अस्त्रशस्त्रों को चलाने में कंप्यूटरों की सहायता ली जा रही है। हाल ही में इराक और अमेरिका के बीच हुए युद्ध में कंप्यूटरों ने इस प्रकार की भूमिका निभाई कि मानव उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मिसाइल छोड़ने में कंप्यूटरों का खुलकर प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से भारी तोपों, वायुयानों, हैलीकॉप्टरों, समुद्री जहाज़ों और पनडुब्बियों के संचालन में भी इनका खुलकर प्रयोग किया जा रहा है।
इस क्षेत्र में अमेरिका ने आशातीत प्रगति की है। सर्वप्रथम अमेरिका में एटम बम से संबंधित गणनाओं के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। लेकिन अब वह इसकी सहायता से ‘स्टार वार्स’ की योजना भी बना रहा है। युद्ध के क्षेत्र में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। चित्रकार भी अब कंप्यूटरों का उपयोग करने लगे हैं। वे अब रंग, कैनवास और कूचियों के अधीन नहीं रहे। अब वे कंप्यूटरों की सहायता से बटन दबाते ही इच्छित रंगों के साथ कागज़ पर चित्र तैयार कर लेते हैं। इन चित्रों की स्वच्छता और कलात्मकता मानव द्वारा बनाए गए चित्रों से श्रेष्ठ होती है। संगीत तथा गीतों की रिकार्डिंग में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है।
महिलाओं के लिए कंप्यूटर का प्रयोग काफी लाभकारी है। यूरोप में महिलाएं अपने अधिकतर गृह-कार्य इन्हीं की सहायता से कर रही हैं। आज मानव-जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ कंप्यूटर की उपयोगिता न हो। रेल और वायुयान यात्रा के लिए टिकटों के आरक्षण की सुविधा कंप्यूटर से सुलभ हो गई है। भारत में भी इसका उपयोग खुलकर होने लगा है। विशेषकर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े-बड़े नगरों में रेलवे स्टेशनों पर निरंतर कंप्यूटर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से परीक्षा परिणाम, मौसम की जानकारी, चुनाव परिणाम, अनुवाद-कार्य, वैज्ञानिक-शोध आदि क्षेत्रों में कंप्यूटरों का प्रयोग काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

45. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
अथवा
मेरा प्रिय नेता
संकेत : भूमिका, जन्म, प्रारंभिक शिक्षा, विदेश-गमन, दक्षिणी अफ्रीका के लिए प्रस्थान, स्वदेश आगमन, ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, महान बलिदान।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं, अपितु संसार के महान पुरुष थे। वे आज के युग की महान विभूति थे। वे सत्य . और अहिंसा के अनन्य पुजारी थे और इन्हीं के प्रयोग से उन्होंने सदियों से गुलाम भारतवर्ष को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाया। संसार में यह एकमात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेज़ों को भी झुकना पड़ा। आने वाली पीढ़ियाँ निश्चय से गौरव के साथ उनका नाम याद करती रहेंगी।
इस युग-पुरुष का जन्म गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्तूबर, 1869 को हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद उनके पिता का नाम था जो राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी का बाल्यकाल राजकोट में व्यतीत हुआ। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था जो एक सती-साध्वी और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थीं। युवा गांधी पर अपनी माता के संस्कारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा।
बालक मोहनदास की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। कक्षा में वे एक साधारण विद्यार्थी थे। वे अपने सहपाठियों से बहुत कम बोलते थे परंतु अपने शिक्षकों का पूरा आदर करते थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा स्थानीय विद्यालय से उत्तीर्ण की। तेरह वर्ष की अल्पायु में ही कस्तूरबा से उनका विवाह हो गया। गांधी जी आरंभ से ही सत्यप्रिय और मेहनती थे। वे कभी भी कोई बात छिपाते नहीं थे।
जिस समय युवा मोहनदास कानूनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए, उस समय वे एक पुत्र के पिता बन चुके थे। विदेश जाने से पूर्व गांधी जी ने अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वे इंग्लैंड जाकर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अपनी माता को दिए वचनों को उन्होंने पूरा पालन किया। इंग्लैंड में उन्होंने असंख्य बाधाओं का सामना किया। शाकाहारी भोजन के लिए उनको अनेक कष्ट झेलने पड़े। अंततः वकालत की शिक्षा पूरी करके ही वे विदेश से लौटे।
जब गांधी जी मुंबई में वकालत कर रहे थे तो वहीं से एक मुकद्दमे के संबंध में उनको दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा लेकिन वहाँ जाकर उनको पता लगा कि वहाँ पर बसे हुए भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। गांधी जी इसे सहन नहीं कर सके। उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। अतः उन्होंने सबसे पहले यहीं पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। इसमें गांधी जी को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ गांधी जी ने नेशनल काँग्रेस की स्थापना भी की।
सन 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। उस समय अंग्रेज़ों का दमन-चक्र जोरों पर था। रौलट एक्ट जैसा काला कानून लागू था। सन 1919 में जलियाँवाला बाग का विनाशकारी कांड हुआ, जिसने समूची मानव जाति को लज्जित कर दिया। धीरे-धीरे अंग्रेज़ों के अत्याचारों में और अधिक वृद्धि होने लगी परंतु यह वह युग था जबकि कुछ शिक्षित लोग ही काँग्रेस सदस्य थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उस समय प्रमुख नेता थे। काँग्रेस पार्टी की स्थिति अधिक मज़बूत न थी। कारण यह था कि काँग्रेस में गरम दल और नरम दल के कारण विभाजन था। जब गांधी जी ने काँग्रेस की बागडोर अपने हाथों में पकड़ी तो देश में एक नए इतिहास का सूत्रपात हुआ। सन 1920 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। पुनः, सन 1928 में जब साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ तो गांधी जी ने उसका डटकर सामना किया। इससे देशभक्तों को काफी प्रोत्साहन मिला। सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन और दांडी यात्रा ने तो अंग्रेज़ों की जड़ों को हिलाकर रख दिया।
सन 1942 में द्वितीय महायुद्ध का अंत हुआ। जब अंग्रेज़ दिए हुए वचन से पीछे हट गए तो गांधी जी ने “अंग्रेज़ो! भारत छोड़ो” का नारा लगाया। गांधी जी ने कहा कि यह मेरी अंतिम लड़ाई है। असंख्य भारतवासियों को जेलों में लूंस दिया गया।
गांधी जी ने भी अपने साथियों के साथ गिरफ्तारी दी। सारे देश में अशांति फैल गई। अंग्रेज़ सरकार भी घबरा गई लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन निरंतर चलता रहा। वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे।
अंततः 15 अगस्त, 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के समक्ष अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा परंतु जाते-जाते अंग्रेज़ फूट के बीज बो गए थे। परिणामस्वरूप भारत-पाक विभाजन हुआ। इस बँटवारे के कारण देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। प्रतिदिन भारत और पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान भेड़-बकरियों की तरह कटने लगे। गांधी जी ने स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को समझाया और सांप्रदायिकता की इस आग को शांत किया। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए उपवास भी रखा।
जब तक गांधी जी जीवित रहे, वे देश के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने छुआछूत को जड़ से उखाड़ने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने अछूत कहे जाने वाले लोगों को ‘हरिजन’ की संज्ञा दी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर अधिक बल दिया तथा खादी वस्त्रों के प्रचार के लिए भरसक प्रयास किया।
लेकिन कुछ भारतीय लोग ही गांधी जी की हिंदू-मुस्लिम एकता की भावना के विरुद्ध थे। 30 जनवरी, 1948 को जब वे दिल्ली स्थित बिरला भवन में प्रार्थना सभा में आ रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उस समय उनके मुख से ‘हे राम!’ के शब्द निकले। उनकी मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सारा देश शोक-सागर में डूब गया। इस प्रकार से अहिंसा के इस महान पुजारी का अंत हो गया।

46. मेरा प्रिय कवि/साहित्यकार
अथवा
महाकवि तुलसीदास
संकेत : भूमिका, जन्म एवं काल, प्रमुख रचनाएँ, विषय की व्यापकता एवं प्रबंध योजना, महान समन्वयवादी चिंतक, सच्चे राम-भक्त, कला-पक्ष।
साहित्य समाज का दर्पण है और लेखक युगद्रष्टा होता है। वह अपने आस-पास की परिस्थितियों से प्रेरित होकर साहित्य की रचना करता है। महाकवि ही श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर सकते हैं। श्रेष्ठ साहित्य के तीन उद्देश्य होते हैं-सत्यं, शिवं एवं सुंदरं। भक्ति काल के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ही युग प्रवर्तक एवं समन्वयवादी कवि थे जिन्होंने अपने साहित्य द्वारा समाज में आदर्शों की स्थापना की और हिंदू धर्म तथा जाति का उद्धार किया। मेरे प्रिय कवि महाकवि एवं रामभक्त तुलसीदास ही हैं। भारत में महात्मा बुद्ध के पश्चात यदि कोई दूसरा समन्वयकारी एवं युगद्रष्टा व्यक्ति हुआ है तो वह महाकवि तुलसीदास ही हैं। आज बड़े-बड़े राजाओं का साम्राज्य नष्ट हो चुका है लेकिन उस महाकवि का साम्राज्य आज भी विद्यमान है।
तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में श्रावण सप्तमी के दिन बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दूबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण माता-पिता ने इनको त्याग दिया और पालन-पोषण के लिए एक दासी को दे दिया। पाँच वर्ष की आयु में उस दासी की मृत्यु हो गई और ये दर-दर भटकने लगे। तत्पश्चात, इनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हुई। वे इन्हें अयोध्या ले गए और उन्होंने इनका नाम ‘रामबोला’ रखा। बालक तुलसीदास दीक्षित होकर विद्याध्ययन करने लगे। काशी में 15 वर्षों तक रहकर इन्होंने वेदों आदि का समुचित अध्ययन किया। गोस्वामी की पत्नी का नाम रत्नावली था।
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 37 मानी गई है, लेकिन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित ‘तुलसी ग्रंथावली’ के अनुसार इनके बारह ग्रंथ ही प्रामाणिक हैं। ये हैं-रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, रामलला नहछू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। गोस्वामी जी की कीर्ति का आधार स्तंभ तो ‘रामचरितमानस’ ही है। इस महाकाव्य का आधार ‘वाल्मीकि रामायण’ है।
तुलसीदास ने व्यापक काव्य-विषय ग्रहण किए हैं। कृष्णभक्त कवियों के समान उन्होंने जीवन के किसी अंग विशेष का वर्णन न करके उसके समग्र रूप को ग्रहण किया। उनकी रचनाओं में शृंगार, शांत, वीर आदि सभी रसों का परिपाक है। उनके द्वारा रचित ‘रामचरितमानस’ में धर्म, संस्कृति तथा काव्य सभी का आश्चर्यजनक समन्वय है। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता प्रबंध योजना
है। उनकी लगभग सभी रचनाओं में कथासूत्र पाए जाते हैं। ‘रामचरितमानस’ की प्रबंध-पटुता तो सर्वश्रेष्ठ है। चार-चार वक्ताओं द्वारा वर्णित होने पर भी उसमें कहीं पर भी अस्पष्टता नहीं आने पाई। समूची कथा मार्मिक प्रसंगों से भरी पड़ी है। कथानक, वस्तु-वर्णन, व्यापार-वर्णन, भाव-प्रवणता और संवाद सभी में पूरा संतुलन है। राम-सीता का परस्पर प्रथम दर्शन, राम वन-गमन, दशरथ की मृत्यु, भरत का पश्चात्ताप, सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि अनेक ऐसे मार्मिक स्थल हैं जिनके कारण ‘रामचरितमानस’ की प्रबंध योजना काफी प्रभावोत्पादक बन पड़ी है।
__गोस्वामी तुलसीदास एक महान समन्वयवादी चिंतक भी थे। उन्होंने दर्शनशास्त्र के शुष्क एवं नीरस सिद्धांतों को भावमय बना दिया। उनके काव्य की महान उपलब्धि उनकी समन्वय भावना है। उन्होंने समाज में व्याप्त विषमता को मिटाकर उसमें एकरूपता उत्पन्न करने का प्रयास किया। धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया। डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में उचित ही कहा है-“तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट् चेष्टा है। रामचरितमानस शुरु से आखिर तक समन्वय का काव्य है।”
तुलसीदास राम काव्यधारा के प्रधान कवि हैं। वस्तुतः उनकी रचनाओं के कारण ही राम काव्यधारा श्रेष्ठ काव्यधारा मानी जाती है। वे कवि होने के साथ-साथ सच्चे रामभक्त भी थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति की स्थापना की। वे अपने आपको दीन और राम को दयालु, स्वयं को भिखारी और भगवान को दानी घोषित करते हैं। तुलसी की भक्ति के कारण ही आज ‘रामचरितमानस’ प्रत्येक हिंदू घर में उपलब्ध है और स्थान-स्थान पर रामायण का पाठ होता है।
तुलसी के काव्य का आंतरिक पक्ष जितना उज्ज्वल है, उसका बाह्य पक्ष भी उतना ही श्रेष्ठ है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उन्होंने अपने समय में प्रचलित अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएँ लिखीं। ‘रामचरितमानस’ में यदि अवधी का सुंदर प्रयोग है तो ‘विनय पत्रिका’ में साहित्यिक ब्रज भाषा का। कहीं-कहीं अरबी और फारसी शब्दों का भी सुंदर मिश्रण है। इनकी भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। कुछ स्थानों पर प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग है। पदों की दृष्टि से तुलसी का क्षेत्र व्यापक है। ‘रामचरितमानस’ में अगर दोहा-चौपाई का प्रयोग है तो ‘कवितावली’ में छंदों की भरमार है। कवित्त, सवैया, दोहा, गीति आदि छंदों का सुंदर प्रयोग है। तुलसी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है परंतु यह अलंकार प्रयोग पूर्णतया स्वाभाविक रूप में हुआ है।
47. अंतरिक्ष यात्री-कल्पना चावला
सकेत : भूमिका, जन्म एवं शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा, प्रथम सफल अंतरिक्ष उड़ान, दूसरी और अंतिम उड़ान, उपसंहार।
भारतवर्ष महान पुरुषों और महिलाओं की भूमि है। यहाँ अनेक महान विभूतियों ने जन्म लेकर संसार में भारत के नाम को उज्ज्वल किया। कल्पना चावला भी उन्हीं में से एक महिला थी। आज के वैज्ञानिक इतिहास में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। वे भारत की ही नहीं बल्कि समूचे एशिया की प्रथम अंतरिक्ष महिला के रूप में जानी जाती हैं। आज भारत के प्रत्येक घर में उनका नाम बड़े आदर-सम्मान के साथ लिया जाता है। बाल्यावस्था से ही उनके मन में सितारों तक पहुँचने का सपना था। स्कूली शिक्षा के काल में वे चाँद-सितारों और अंतरिक्ष के चित्र बनाती थीं। उनका सपना साकार हुआ और उन्होंने दो बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। कल्पना चावला का एकमात्र लक्ष्य था-अंतरिक्ष यात्री बनना लेकिन वे जीवंत स्वभाव की महिला थीं। भारत के शास्त्रीय संगीत से उन्हें अत्यधिक लगाव था।
कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के एक छोटे-से नगर करनाल में 1 जुलाई, 1961 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री बनारसीदास चावला तथा माता का नाम श्रीमती संयोगिता देवी चावला है। कल्पना की दो बहनें और एक भाई हैं। अपने भाई-बहनों में वे सबसे छोटी थीं। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा करनाल के स्थानीय विद्यालय टैगोर बाल निकेतन में प्राप्त की। दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कल्पना ने प्री-इंजीनियरिंग की शिक्षा स्थानीय दयाल सिंह कॉलेज से प्राप्त की। बाद में कल्पना चावला ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1982 में उन्होंने एम०एस-सी० करने के लिए अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1988 के लगभग कल्पना चावला का विवाह अमेरिका के नागरिक ज्यां पियरे हैरिस से हुआ। अपने पति तथा मित्रों से प्रेरणा प्राप्त कर वे अंतरिक्ष विज्ञान में अधिकाधिक रुचि लेने लगीं।
कल्पना चावला को बचपन से ही हवाई जहाज के मॉडल बनाने का बहुत शौक था। आरंभ से ही उनके मन में अंतरिक्ष यात्री . बनने का संकल्प था। कल्पना चावला ने पायलट का लाइसेंस 1988 से 1994 के बीच सान फ्रांसिस्को में रहते हुए प्राप्त किया था। बाद में उन्होंने कलाबाजी उड़ान भी सीखी। कल्पना चावला के कैरियर की शुरुआत नासा एमेस शोध केंद्र में हुई। कैलीफोर्निया में उन्होंने एक शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। 1994 में उन्हें नासा के लिए चुन लिया गया। यहाँ एक वर्ष तक कठोर परीक्षण प्राप्त करने के बाद वे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुन ली गईं।
मार्च, 1995 में कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के 15वें समूह के उम्मीदवार के रूप में जॉनसन स्पेस सैंटर में भेज दी गईं। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। 1996 में कल्पना चावला ने वास्तविकता में छलांग लगाई और उन्हें मिशन विशेषज्ञ का दर्जा प्राप्त हुआ। 19 नवंबर, 1997 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान द्वारा उन्होंने अपनी प्रथम अंतरिक्ष उड़ान भरी। यह यान 17 दिन, 16 घंटे और 33 मिनट तक अंतरिक्ष में रहा। जब वे अपनी सफल उड़ान भरकर लौटीं तो उनके चेहरे पर सफलता की खुशी छाई हुई थी। इस उड़ान के बाद तो कल्पना चावला ने अपना समूचा जीवन ही अंतरिक्ष उड़ान विज्ञान को समर्पित कर दिया।
दूसरी बार कल्पना चावला को अंतरिक्ष यान कोलंबिया की शुद्ध उड़ान-एसटीएस-107 के लिए चुन लिया गया। इस उड़ान काल में उनके साथ छह अन्य वैज्ञानिक भी थे। वे अंतरिक्ष में 16 जनवरी, 2003 को गईं। 16 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद जब वे 1 फरवरी, 2003 को धरती की ओर लौट रही थीं, तब 25 लाख पुों वाली चमत्कारी उड़ान मशीन कोलंबिया अंतरिक्ष में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
टेक्सास-अरकंसास और लुसियाना के ऊपर कोलंबिया के अनेक टुकड़े बिखर गए और साहसी युवती कोलंबिया के विस्फोट में अपने छह अन्य साथियों के साथ इस संसार से विदा हो गई। कल्पना ने इस उड़ान में अंतरिक्ष में 760 घंटे बिताए तथा पृथ्वी के 252 चक्कर काटे। संभवतः विधाता को यह स्वीकार नहीं था कि यह युवती लौटकर फिर से भारत आती। कल्पना की कहानी दूसरे भारतीयों की सफलता की आम कहानियों की तरह नहीं थी। वीर नायिका की तरह अपना सपना पूरा करते हुए ही उसकी मृत्यु हुई लेकिन इस मृत्यु ने उसे राष्ट्रीय नायिका बना दिया।
यद्यपि कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त थी तथापि उनके मन में अपने देश के प्रति अत्यधिक प्रेम . था। करनाल नगर के निवासियों, विशेषकर, टैगोर बाल निकेतन विद्यालय से उन्हें अत्यधिक प्यार था। यही कारण है कि करनाल के इस विद्यालय से प्रतिवर्ष दो विद्यार्थी नासा में आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के बच्चों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा था-“भौतिक लाभ ही प्रेरणा के स्रोत नहीं होने चाहिएँ। ये तो आप आगे भी हासिल कर सकते हैं। मंजिल तक पहुँचने का रास्ता तलाशिए। सबसे छोटा रास्ता ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। मंजिल ही नहीं, उस तक का सफर भी अहमियत रखता है……….।”

48. गणतंत्र दिवस
अथवा
गणतंत्र दिवस आयोजन
संकेत : भूमिका, स्वतंत्रता पूर्व स्थिति, भारत का गणतंत्र राज्य घोषित होना, राष्ट्र का पावन पर्व, दिल्ली में गणतंत्र, उपसंहार।
31 दिसंबर, 1928 को श्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासकों को चुनौती दी थी, “यदि ब्रिटिश सरकार हमें औपनिवेशिक स्वराज देना चाहे तो 31 दिसंबर, 1929 तक दे दे।” परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस इच्छा की पूर्ण अवहेलना कर दी। सन 1930 में लाहौर में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। श्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रावी नदी के तट पर बहुत विशाल पंडाल बनाया गया था। उस अधिवेशन में 26 जनवरी, 1930 की रात को श्री नेहरू ने घोषणा की कि “अब हमारी मांग पूर्ण स्वतंत्रता है और हम स्वतंत्र होकर रहेंगे।”
उस दिन भारत के गाँव-गाँव और नगर-नगर में स्वतंत्रता की शपथ ली गई। जगह-जगह सभाएँ की गईं, जुलूस निकाले गए, करोड़ों भारतीयों के कंठों से एक साथ गर्जना हुई, “आज से हमारा लक्ष्य है-पूर्ण स्वाधीनता। जब तक हम पूर्ण स्वाधीन नहीं हो जाएँगे, तब तक निरंतर बलिदान देते रहेंगे।”
ब्रिटिश शासनकाल में 26 जनवरी, 1930 के बाद से लेकर प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन स्थान-स्थान पर सभाएँ करके लाहौर में रावी नदी के तट पर की गई पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा दोहराई जाती थी। इधर भारतीयों ने पूर्ण स्वाधीनता की प्रतिज्ञा की, उधर ब्रिटिश सरकार ने अपना दमन-चक्र जोरदार ढंग से चला दिया। लाठियों से स्वाधीनता-प्रेमियों के सिर फोड़े जाने लगे। कई जगह गोलियाँ चलाई गईं और देशप्रेमियों को भूना जाने लगा। कई नेताओं को जेलों में डाला जाने लगा परंतु भारतीय अपने पथ पर अडिग रहे। भयानक-से-भयानक यातनाएँ भी उन्हें अपने पथ से विचलित न कर सकीं। उसी अविचल देशभक्ति का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी सभ्यता देश के स्वतंत्र वातावरण में साँस ले रहे हैं।
सन 1950 में जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, तब यह विचार किया गया कि किस तिथि से इसे भारतवर्ष में लागू किया जाए। गहन विचार-विमर्श के पश्चात 26 जनवरी ही इसके लिए उपयुक्त तिथि समझी गई। अतः 26 जनवरी, 1950 को भारतवर्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र घोषित कर दिया गया। देश का शासन पूर्ण रूप से भारतवासियों के हाथों में आ गया। प्रत्येक नागरिक देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगा। देश की उन्नति तथा इसकी मानमर्यादा को प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति तथा मान-मर्यादा समझने लगा। भारत के इतिहास में वास्तव में यह दिन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
26 जनवरी हमारे राष्ट्र का एक पुनीत पर्व है। असंख्य बलिदानों की पावन स्मृति लेकर यह हमारे सामने उपस्थित होता है। कितने ही वीर भारतीयों ने देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों को हँसते-हँसते चढ़ा दिया। कितनी ही माताओं ने अपनी गोद की शोभा, कितनी ही पत्नियों ने अपनी माँग का सिंदूर और कितनी ही बहनों ने अपना रक्षा-बंधन का त्योहार हँसते-हँसते स्वतंत्रता संग्राम को भेंट कर दिया। आज के दिन हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अपने खून की आहुति दी थी।
गणतंत्र दिवस सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस दिन की शोभा अनुपम होती है। इस दिन की शोभा देखने के लिए देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से लोग उमड़ पड़ते हैं। 26 जनवरी को इंडिया गेट के मैदान में जल, थल और वायु सेनाओं की टुकड़ियाँ राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। 31 तोपें दागी जाती हैं। सैनिक वाद्य यंत्र बजाते हैं। राष्ट्रपति अपने भाषण में राष्ट्र को कल्याणकारी संदेश देते हैं। भिन्न-भिन्न प्रांतों की मनोहारी झाँकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। रात को सारी राजधानी विद्युत् दीपों के प्रकाश से जगमगा उठती है।
देश के अन्य सभी राज्यों में भी इस प्रकार के पावन समारोहों का आयोजन किया जाता है। खेल, तमाशे, सजावट, सभाएँ, भाषण, रोशनी, कवि-गोष्ठियाँ, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। सरकार तथा जनता दोनों ही इस मंगल पर्व को मनाते हैं। सारे देश में प्रसन्नता और हर्ष की लहर दौड़ जाती है। यह पर्व हमारे राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन देश की विभिन्न राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। ये झांकियाँ हमें अनेकता में एकता का संदेश देती हैं।
वास्तव में, 26 जनवरी एक महिमामयी तिथि है। इसके पीछे भारतीय आत्माओं के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी निहित है जो सदैव भावी संतान को अमर प्रेरणा देती रहेगी। भारतीय इतिहास में यह दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। प्रत्येक भारतीय का यह परम कर्तव्य है कि वह इस पर्व को उल्लास तथा आनंद के साथ मनाए और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहे परंतु स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम पारस्परिक भेदभाव को भूलकर सहयोग और एकता में विश्वास करें। यदि हम अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाशपूर्ण मार्ग पर अग्रसर होंगे, तभी हम इस महिमामयी तिथि की मान-मर्यादा दृढ़ रख सकेंगे।

49. ऋतुराज बसंत
अथवा
बसंत पंचमी
संकेत : ऋतुओं का राजा, सुहावना मौसम, प्राणी जगत में उल्लास, बसंत पंचमी, ऐतिहासिक महत्त्व।
भारत अपनी प्राकृतिक शोभा के लिए प्रसिद्ध है। इसे ऋतुओं का देश कहा जाता है। भारतवासी धन्य हैं, जो उस धरती पर रहते हैं, जहाँ षऋतुओं का नियमित क्रम सदा गतिशील रहता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर-इन सबका अपना महत्त्व है तथा इनका चक्र स्वच्छंद गति से चलता रहता है। ये ऋतुएँ बारी-बारी से आती हैं, अपनी छटा दिखाती हैं तथा भारत माँ का शृंगार करती हैं और चली जाती हैं। सभी ऋतुओं की अपनी-अपनी शोभा है, परंतु बसंत ऋतु की शोभा सबसे निराली है। ऋतुओं में इसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है इसलिए इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है।
बसंत ऋतु का आगमन शिशिर और पतझड़ के बाद होता है। वैसे तो बसंत ऋतु फाल्गुन मास से प्रारंभ हो जाती है, किंतु इसके वास्तविक महीने चैत्र और वैशाख हैं। 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक का समय बसंत काल कहलाता है। इस समय मौसम बहुत सुहावना होता है, न अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। प्रकृति के प्रत्येक अंग पर बसंत का प्रभाव दिखाई देने लगता है। पौधों, वृक्षों, लताओं आदि पर नए-नए पत्ते निकलते हैं, सुंदर फूल खिलने लगते हैं, रंग-बिरंगी तितलियाँ उड़ने लगती हैं, आम बौराते हैं और अपनी सुगंध से वातावरण को महका देते हैं। पीली-पीली सरसों फूलने लगती है। बसंत ऋतु प्रकृति के लिए वरदान लेकर आती है। पृथ्वी का कण-कण एक नए आनंद, उत्साह और संगीत का अनुभव करता है।
प्राणी जगत में भी यह ऋतु उल्लास और उमंग का संचार करती है। पशु-पक्षी जोश, उत्साह और प्रेम से भर जाते हैं। कोयलें, चकवे और भौरे विशेष रूप से मतवाले हो उठते हैं। कोयल का मधुर स्वर अमराइयों में गूंजने लगता है। मनुष्य जाति उमंग से भर जाती है। किसान का मन अपनी लहलहाती खेती देखकर झूमने लगता है। कवि तथा कलाकार इस ऋतु से विशेष प्रभावित होते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इस ऋतु का अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर में नए रक्त का संचार होता है तथा स्वास्थ्य की उन्नति होती है।
बसंत ऋतु में दिशाएँ साफ हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाता है। चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। जड़ में भी चेतना आ जाती है। सूर्य की तीव्रता भी अधिक नहीं होती। दिन-रात एक समान होते हैं। इन दिनों वायु प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह वायु दक्षिण की ओर से आती है, इसलिए इसे ‘दक्षिण-पवन’ कहते हैं। यह शीतल, मंद, मतवाली और सुगंधित होती है। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने झूमती हुई बसंती हवा का वर्णन इन शब्दों में किया है
“हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ,
सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ,
बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्तमौला।”
बसंत ऋतु का आगमन गुरु गोबिंद सिंह जी के उन अबोध वीर बालकों की याद दिलाता है, जिनके खून से चमकौर के दुर्ग की मिट्टी आज भी रंगी दिखाई देती है। इन वीरों की याद में फाल्गुन की पंचमी के दिन बसंत पंचमी का मेला लगता है। बसंत-पंचमी इस ऋतु का प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और चारों ओर सुख एवं प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस दिन प्रातः पौ फटने से लेकर रात गए तक लोग अपने घरों पर और मैदानों में जाकर पतंग उड़ाते हैं। पूरा आकाश पतंगों से भरा होता है। होली भी बसंत ऋतु का त्योहार है। इस दिन अबीर और गुलाल तथा रंगों से भी पिचकारियाँ लोगों के तन-मन को रंग देती हैं। सारा वातावरण रंगीन बन जाता है। सभी आनंद में मगन हो जाते हैं।
बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्म हुआ। इसलिए इस दिन सरस्वती पूजन भी किया जाता है। इस पवित्र दिन वीर हकीकत राय का बलिदान हुआ था। वीर हकीकत राय के बलिदान के कारण इस दिन का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। वीर हकीकत राय का बलिदान हमें अपने धर्म पर अटल और अडिग रहने का संदेश देता है। सभी धर्म पवित्र हैं तथा प्रेरणा देते हैं कि किसी भी धर्म के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। हकीकत राय अपने धर्म के प्रति अडिग रहे और शहीद हो गए। उनकी याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है। वीर हकीकत के बलिदान को याद करके एक ओर तो दुःख होता है, परंतु साथ ही सभी धर्मों को एक समान मानने वालों का सीना गर्व से फूल जाता है।
इस प्रकार बसंत ऋतु प्रकृति का एक वरदान है। इसे मधुमास भी कहा जाता है। इसका सौंदर्य अद्भुत व अद्वितीय है। कहा भी गया है
‘आ आ प्यारी बसंत सब ऋतुओं से प्यारी। तेरा शुभागमन सुनकर फूली केसर क्यारी।।’
50. समाचार-पत्रों का महत्त्व
संकेत : भूमिका, भारत में समाचार-पत्र का आरंभ, जन-जागरण का माध्यम, समाचार-पत्रों के लाभ, समाचार पत्रों से हानियाँ, उपसंहार।
विज्ञान ने विश्व को बहुत छोटा बना दिया है। आवागमन के साधनों के कारण स्थानीय दूरियाँ भी समाप्त हो चुकी हैं लेकिन रेडियो, दूरदर्शन और समाचार-पत्रों ने सारे संसार को एक परिवार बना दिया है। अब हम अपने घर में बैठे-बैठे दूर देशों की ख़बरें पढ़ लेते हैं तथा सुन लेते हैं। हमें दूसरे देशों अथवा राज्यों में जाना नहीं पड़ता। हमें घर बैठे ही संसार के सारे समाचार मिल जाते हैं। कहाँ क्या घटित होता है अथवा किस देश की गतिविधियाँ क्या हैं हमें इसका पता समाचार-पत्रों से ही लगता है। आज के जीवन में जितना महत्त्व रोटी और पानी का है, उतना ही समाचार-पत्र का भी है। प्रातःकाल उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले समाचार-पत्र की ओर जाता है। जिस दिन भी हम समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, हमारा वह दिन सूना-सूना प्रतीत होता है।
भारत में सबसे पहले जिस समाचार-पत्र का प्रकाशनं आरंभ हुआ था, उसका नाम था-‘समाचार-दर्पण’ । बाद में ‘उदंत मार्तंड’ का प्रकाशन आरंभ हुआ। तत्पश्चात, 1850 में राजा शिवप्रसाद ‘सितारेहिंद’ ने ‘बनारस अखबार’ निकाला। इसके बाद तो भारत में पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़-सी आ गई। ज्यों-ज्यों मुद्रण-कला का विकास होने लगा, त्यों-त्यों समाचार-पत्रों की संख्या भी बढ़ने लगी।
आज देश के प्रत्येक भाग में समाचार-पत्रों का प्रकाशन हो रहा है। कुछ ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्र भी हैं जिनका प्रकाशन नियमित रूप से हो रहा है। दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी हिंदी भाषा में प्रकाशित कुछ प्रसिद्ध समाचार-पत्र हैं। इसी प्रकार से अंग्रेज़ी में The Tribune, The Hindustan Times, Times of India, Indian Express आदि समाचार-पत्र भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं परंतु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि आज समाचार-पत्रों का उद्योग एक स्थानीय उद्योग बन चुका है, जिससे लाखों लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।
समाचार-पत्र केवल समाचार ही नहीं पहुँचाते, बल्कि ये जन-जागरण का भी माध्यम हैं। ये मानव-जाति को समीप लाने का भी काम करते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, वहाँ इनका विशेष महत्त्व है। ये लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराते हैं। समाचार-पत्र सरकार के उन कामों की कड़ी आलोचना करते हैं जो देश के लिए या जनसाधारण के लिए लाभकारी नहीं हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि दो-चार समाचार-पत्रों को छोड़कर शेष सभी अपने दायित्व को अच्छी प्रकार से निभा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में हमारे देश के समाचार-पत्रों ने अच्छी भूमिका निभाई और अन्याय तथा अत्याचार का डटकर विरोध किया।
समाचार-पत्र समाज के लिए लाभकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संसार के लोगों में आपसी भाईचारे और मानवता की भावना उत्पन्न करते हैं, साथ ही, सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। यही नहीं, ये लोगों में देशप्रेम की भावना भी उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्ति की स्वाधीनता और उसके अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। चुनाव के दिनों में समाचार-पत्रों की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। आज संसार में किसी भी प्रकार की शासन-पद्धति क्यों न हो लेकिन समाचार-पत्रों ने ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई है।
अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध समाचार-पत्रों ने ही जनमत तैयार किया था। इसी प्रकार से अनेक समाचार-पत्रों के संपादकों और पत्रकारों ने अन्याय का विरोध करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। ‘पंजाब केसरी’ के संपादक लाला जगत नारायण का बलिदान आज भी हमारे मन में उनकी याद को ताज़ा करता है। यही नहीं, समाचार-पत्र विज्ञापन का भी सशक्त माध्यम हैं। उपभोग की विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन इनमें ही छपते हैं। विभिन्न नौकरियों के विज्ञापन भी इनमें छपते रहते हैं। इसी प्रकार से शैक्षणिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टियों से भी समाचार-पत्रों का काफी महत्त्व है।
समाचार-पत्रों से लाभ तो अनेक हैं परंतु कुछ हानियाँ भी हैं। समाचार-पत्र पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। अतः कभी-कभी ये झूठे और बेबुनियादी समाचार छापने लग जाते हैं। कभी-कभी ये सच्चाई को तोड़-मरोड़कर छाप देते हैं। इसी प्रकार से सांप्रदायिकता का विष फैलाने में भी कुछ समाचार-पत्र भाग लेते हैं। समाज को लूटने वाले और प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर वे उनके विरुद्ध कुछ नहीं लिखते। इससे समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय को बल मिलता है। कुछ समाचार-पत्र पूँजीपतियों की संपत्ति हैं।
अतः उनसे न्याय, मंगल और सच्चाई की तो आशा ही नहीं की जा सकती। कुछ संपादक और संवाददाता अमीरों तथा राजनीतिज्ञों के हाथों में बिककर उलटे-सीधे समाचार छापकर जनता को गुमराह करते हैं।
जो वस्तु जितनी अधिक महत्त्वपूर्ण होती है, उसका दायित्व भी उतना ही अधिक होता है। समाचार-पत्र स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष, सत्य के पुजारी और निरंतर जागरूक हों, यह आवश्यक है। ये जनसाधारण की वाणी हैं। ऐसी स्थिति में उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। समाज में फैले हुए अत्याचार, अनाचार, अन्याय और अधर्म का विरोध करना समाचार-पत्रों का ही दायित्व है। इसी प्रकार से रूढ़ियों, कुप्रथाओं और कुरीतियों का उन्मूलन करने में भी समाचार-पत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाचार-पत्रों का अत्यधिक महत्त्व है।

51. नैतिक शिक्षा का महत्त्व
संकेत : भूमिका, अंग्रेज़ी शिक्षण पद्धति का प्रारंभ, प्राचीन शिक्षा-पद्धति, नैतिक शिक्षा का अर्थ, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, उपसंहार।
मानव जन्म से ही सुख और शांति के लिए प्रयास करता आया है। अपनी उन्नति के लिए वह सृष्टि के आरंभ से ही प्रयत्नशील है, परंतु उसे पूर्ण शांति शिक्षा द्वारा ही प्राप्त हुई है। शिक्षा का अस्त्र अमोघ है। इससे ही मानव की सामाजिक और नैतिक उन्नति हुई और वह आगे बढ़ने लगा। मानव को अनुभव होने लगा कि शिक्षा के बिना वह पशुतुल्य है। शिक्षा ही मानव को उसके कर्तव्यों से परिचित कराती है, उसे सही अर्थों में इंसान बनाती है और उसे अपना तथा समाज का विकास करने का अवसर प्रदान करती है।
मानव की सभी शक्तियों के सर्वतोन्मुखी विकास का दूसरा नाम शिक्षा है। इससे मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व का विकास होता है। गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है, “शिक्षा का अर्थ बच्चे की सभी शारीरिक, मानसिक व नैतिक शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास है।” दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा अंग्रेज़ों की विरासत है। अंग्रेज़ भारत को अपना उपनिवेश समझते थे। उन्होंने भारतीयों को क्लर्क और मुंशी बनाने की चाल चली। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेज़ी शिक्षा-प्रणाली के संदर्भ में कहा था-“मुझे विश्वास है कि इस शिक्षा योजना से भारत में एक ऐसा शिक्षित वर्ग बन जाएगा जो रक्त और रंग से तो भारतीय होगा पर रुचि, विचार, वाणी और मस्तिष्क से अंग्रेज़ी।” इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को केवल ‘बाबू’ बना दिया। उन्हें भारतीय संस्कृति से तो दूर रखा ही, अंग्रेज़ी मानसिकता को उनके भीतर गहराई तक पहुंचा दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी हमारे यहाँ इसी प्रणाली का वर्चस्व बना हुआ है।
प्राचीन ऋषियों एवं विचारकों ने यह घोषणा की कि शिक्षा मानव वृत्तियों के विकास तथा आत्मिक शांति के लिए परमावश्यक है। शिक्षा मानव की बुद्धि को परिष्कृत एवं परिमार्जित करती है। शिक्षा से मानव में सत्य और असत्य का विवेक जागृत होता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराना था, उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर करना था और उसमें संस्कारों को उत्पन्न करना था। अतः प्राचीन शिक्षा-पद्धति में नैतिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। प्राचीन काल में यह शिक्षा नगर के कोलाहल और कलरव से दूर सघन वनों में स्थित महर्षियों के गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती थी। छात्र पूरे पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ तथा गुरु के चरणों की सेवा करता हुआ विधिवत विद्याध्ययन करता था। इन पवित्र आश्रमों में विद्यार्थी की सर्वांगीण उन्नति पर ध्यान दिया जाता था। उसे अपनी बहुमुखी प्रतिभा के विकास का अवसर मिलता था। विज्ञान, चिकित्सा, नीति, युद्ध-कला, वेद तथा शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करके विद्यार्थी पूर्ण रूप से विद्वान होकर तथा योग्य नागरिक बनकर अपने घर लौटता था।
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नैतिक शिक्षा है क्या ? नैतिक शब्द नीति में इक् प्रत्यय जुड़ने से बना है। इसका अर्थ है, नीति संबंधी शिक्षा। नैतिक शिक्षा का अर्थ यह है कि विद्यार्थियों को उदारता, न्यायप्रियता, कठोर परिश्रम, कृतज्ञता, सत्यभाषण, सहनशीलता, इंद्रिय निग्रह, विनम्रता, प्रामाणिक आदि सद्गुणों की शिक्षा दी जाए। आज स्वतंत्र भारत में सच्चरित्रता की बड़ी कमी है। सरकारी, और गैर-सरकारी सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अवसरवादिता तथा हिंसा हमारे जीवन में विष घोल रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थी को वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा तो दी जाती है, तकनीकी शिक्षण की भी व्यवस्था है लेकिन उसे सही अर्थों में मानव बनना नहीं सिखाया जाता।
कर्तव्यपालन, विनम्र भाव, संतोष, सादगी, सद्व्यवहार और परोपकार की शिक्षा नहीं दी जाती। यही तो मानव की अमूल्य संपत्ति है जिसके समक्ष धन-संपत्ति आदि तुच्छ हैं। इन्हीं से राष्ट्र का निर्माण होता है और इन्हीं से देश सुदृढ़ होता है।
शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाना, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना, देशवासियों का चरित्र निर्माण करना तथा मनुष्य को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराना है परंतु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से इस प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, यह तो उदरपूर्ति का साधन मात्र बनकर रह गई है। नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। श्रद्धा जैसी कोई भावना रही ही नहीं है। गुरुजनों का आदर नहीं रहा और माता-पिता का सम्मान नहीं रहा। विद्यार्थी वर्ग तो क्या समूचे शिक्षित समाज में अराजकता फैली हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे मन में यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि हमारी शिक्षण-व्यवस्था में क्या कमी है। शिक्षा शास्त्रियों का एक वर्ग इस बात पर बार-बार बल देता रहा है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली में नैतिक शिक्षा के लिए भी स्थान होना चाहिए। कुछ धर्मगुरुओं और धार्मिक महात्माओं ने भी इस बात पर बल दिया है कि नैतिक शिक्षा के बिना हमारी शिक्षा-प्रणाली अधूरी है।
आज के भौतिकवादी युग में नैतिक शिक्षा नितांत आवश्यक है। इसी शिक्षा के फलस्वरूप ही राष्ट्र का सही अर्थों में निर्माण हो सकता है। विशेषकर, आज के युवक-युवतियों के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक शिक्षा को लागू करना ज़रूरी है। इस शिक्षा द्वारा ही सच्चे एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का विकास हो सकता है।

52. भूकंप : एक प्राकृतिक आपदा
सकेत : भूमिका, भूकंप का अर्थ, भूकंप से ग्रस्त क्षेत्र, भूकंप का तांडव नाच, उपसंहार।
मानव आदि युग से प्रकृति के साहचर्य में रहता आया है। प्रकृति के प्रांगण में मानव को कभी माँ की गोद का सुख मिलता है तो कभी वही प्रकृति उसके जीवन में संकट बनकर भी आती है। बसंत की सुहावनी हवा के स्पर्श से जहाँ मानव पुलकित हो उठता है तो वहीं उसे ग्रीष्म ऋतु की जला देने वाली गर्म हवाओं का सामना भी उसे करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को तेज आँधियों, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है।
‘भूकंप’ का अर्थ है भू का काँप उठना अर्थात् पृथ्वी का डाँवाडोल होकर अपनी धुरी से हिलकर और फटकर अपने ऊपर विद्यमान जड़ और चेतन प्रत्येक प्राणी और पदार्थ को विनाश की चपेट में ले लेना तथा सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर देना। जापान में तो अकसर भूकंप आते रहते हैं जिनसे विनाश के दृश्य उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि वहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। भारतवर्ष में भी भूकंप के कारण अनेक बार विनाश के दृश्य उपस्थित हुए हैं। पूर्वजों की जुबानी सुना है कि भारत के कोटा नामक (पश्चिम सीमा प्रांत, अब पाकिस्तान में स्थित एक नगर) स्थान पर विनाशकारी भूकंप आया। यह भूकंप इतनी तीव्र गति से आया था कि नगर तथा आस-पास के क्षेत्रों के हजारों घर-परिवारों का नाम तक भी बाकी नहीं रहा था।
विगत वर्षों में गढ़वाल, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में विनाशकारी भूकंप आया था जिससे वहाँ जन-जीवन तहस-नहस हो गया था। पहले गढ़वाल के क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। वह एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ भूकंप के झटकों के कारण पहाड़ियाँ खिसक गई थीं, उन पर बने मकान भी नष्ट हो गए थे। हजारों लोगों की जानें गई थीं। वहाँ की विनाशलीला से विश्व भर के लोगों के दिल दहल उठे थे। उस विनाशलीला को देखकर मन में विचार उठते हैं कि प्रकृति की लीला भी कितनी अजीब है। वह मनुष्य को बच्चों की भाँति अपनी गोद में खिलाती हुई एकाएक पूतना का रूप धारण कर लेती है। वह मनुष्य के घरों को बच्चों के द्वारा कच्ची मिट्टी के बनाए गए घरौंदों की भाँति तोड़कर बिखरा देती है और मनुष्यों को मिट्टी के खिलौनों की भाँति कुचल डालती है। गढ़वाल के क्षेत्र में भूकंप के कारण वहाँ का जन-जीवन बिखर गया था। कुछ समय के लिए तो वहाँ का क्षेत्र भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों से कट-सा गया था।
इसी प्रकार महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में आए भूकंप के समाचार मिले। यह भूकंप इतना भयंकर और विशाल था कि धरती में जगह-जगह दरारें पड़ गईं। हजारों लोगों की जानें चली गईं। चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई। सरकार की ओर से पहुंचाई जाने वाली सहायता के अतिरिक्त अनेक सामाजिक संस्थाओं और विश्व के अनेक देशों ने भी संकट की इस घड़ी में वहाँ के लोगों की हर प्रकार से सहायता की, किंतु उनके अपनों के जाने के दुःख को कम न कर सके।
धीरे-धीरे समय बीतता गया और समय ने वहाँ के लोगों के घाव भर दिए। वहाँ का जीवन सामान्य हुआ ही था कि 26 जनवरी, 2003 को प्रातः आठ बजे गुजरात में विनाशकारी भूकंप ने फिर विनाश का तांडव नृत्य कर डाला। वहाँ रहने वाले लाखों लोग भवनों के मलबे के नीचे दब गए थे। मकानों के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने का काम कई दिनों तक चलता रहा। कई लोग तो 36 घंटों के बाद भी जीवित निकाले गए थे। वहाँ भूकंप के झटके कई दिनों तक अनुभव किए गए थे। इस प्राकृतिक प्रकोप की घटना से विश्वभर के लोगों के दिल दहल उठे थे। कई दिनों तक चारों ओर रुदन की आवाजें सुनाई देती रहीं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य अपने साधनों के अनुरूप समान रूप से सहानुभूति और सहृदयता दिखा रहे थे तथा पीड़ितों को राहत पहुँचा रहे थे।
यह भूकंप कितना भयानक था इसका अनुमान वहाँ पर हुए विनाश से लगाया जा सकता है। वहाँ के लोगों ने बहुत हिम्मत से काम लिया और अपना कारोबार फिर जमाने में जुट गए। लोग अभी प्रकृति की भयंकर आपदा से उभर ही रहे थे कि 8 अक्तूबर, 2005 को कश्मीर और उससे लगते पाकिस्तान के क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया। संपूर्ण क्षेत्र की धरती काँप उठी थी। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पहाड़ों पर बसे हुए गाँव-के-गाँव तहस-नहस हो गए। साथ ही ठंड सर्दी के प्रकोप ने वहाँ के लोगों को ओर भी मुसीबत में डाल दिया। कड़कती सर्दी में वहाँ के लोगों को खुले मैदानों में रहना पड़ा। सरकार ने हैलीकाप्टरों व अन्य साधनों से वहाँ के लोगों की सहायता के लिए सामान पहुँचाया। भारतीय क्षेत्र की अपेक्षा पाकिस्तान क्षेत्र में अत्यधिक हानि हुई। लाखों लोगों को जान से हाथ धोने पड़े। प्राणियों को जन्म देने वाली और उनकी सुरक्षा करने वाली प्रकृति माँ ही उनकी जान की दुश्मन बन गई थी।
प्राकृतिक प्रकोप के कारण पीड़ित मानवता के प्रति हमें सच्ची सहानुभूति रखनी चाहिए और सच्चे मन से हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जिनके प्रियजन चले गए, हमें उनके प्रति सद्व्यवहार एवं सहानुभूति दिखाते हुए उनके दुःख को कम करना चाहिए। उनके साथ खड़े होकर उन्हें धैर्य बँधाना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ी सहायता होगी।
कितनी अजीब है यह प्रकृति और कैसे अनोखे हैं उसके नियम, यह समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। भूकंप के दृश्यों को देखकर आज भी एक सनसनी-सी उत्पन्न हो जाती है। किन्तु प्रकृति की अजीब-अजीब गतिविधियों के साथ-साथ मानव की हिम्मत और साहस की भी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता कि वह प्रत्येक प्राकृतिक आपदा का सदा ही साहसपूर्वक मुकाबला करता आया है।
53. प्राकृतिक प्रकोप : सुनामी लहरें
प्रकृति का मनोरम रूप जहाँ मनुष्य के विकास के लिए सदा सहायक है, वहाँ भयंकर रूप उसके विनाश का कारण भी बनता रहा है। मानव जहाँ आदिकाल से प्रकृति की गोद में खेलकूद कर बड़ा होता है, वही गोद कभी-कभी उसको निगल भी जाती है। अतिवृष्टि (अत्यधिक वषा), बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान, आँधी आदि प्राकृतिक प्रकोप के विभिन्न रूप हैं। 26 दिसंबर, 2004 को समुद्र में उठी भयंकर लहरें भी विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप था। महाविनाशकारी ‘सुनामी’ की उत्पत्ति भी वास्तव में समुद्रतल में भूकंप आने से होती है। समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भू-स्खलन के कारण यदि बड़े स्तर पर पृथ्वी की सतहें (प्लेटें) खिसकती हैं तो इससे सतह पर 50 से 100 फुट ऊँची लहरें, 800 कि०मी० प्रति घंटे की तीव्र गति से तटों की ओर दौड़ने लग जाती हैं। पूर्णिमा की रात्रि को तो ये लहरें और भी भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। 26 दिसंबर को भूकंप के कारण उठी इन लहरों ने भयंकर रूप धारण करके लाखों लोगों की जाने ले ली और अरबों की संपत्ति को नष्ट कर डाला।
वस्तुतः ‘सुनामी’ शब्द जापानी भाषा का है। जहाँ अत्यधिक भूकंप आने के कारण वहाँ के लोगों को बार-बार प्रकृति के इस प्रकोप का सामना करना पड़ता है। हिंद महासागर के तल में आए भूकंप के कारण ही 26 दिसंबर को समुद्र में भयंकर सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थीं। इस सुनामी तूफान ने चार अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी में ऐसी हलचल मचा दी कि इंडोनेशिया, मालद्वीप, श्रीलंका, मलेशिया, अंडमान, निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र-प्रदेश, केरल आदि सारे तटीय क्षेत्रों पर तबाही का नग्न तांडव हुआ। मछलियाँ पकड़कर आजीविका कमाने वाले कई हजार मछुआरे इस भयंकर सुनामी लहरों की चपेट में आकर जीवन से हाथ धो बैठे। अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों में स्थित वायु-सेना के अड्डे को भी भयंकर क्षति पहुँची तथा सौ से अधिक वायु-सेना के जवान, अधिकारी वर्ग और उनके परिजन काल के ग्रास बन गए। पोर्ट ब्लेयर हवाई पट्टी को क्षति पहुँची। उसकी पाँच हजार फीट की पट्टी सुरक्षित होने से राहत पहुँचाने वाले 14 विमान उतारे गए। इस संकट के समय में भारतीय विमानों को श्रीलंका और मालदीव के लोगों की सहायता के लिए भेजा गया। कई मीटर ऊँची सुनामी लहरों ने निकोबार में ए०टी०सी० टावर को भी ध्वस्त कर डाला था, किंतु तत्काल सचल ए०टी०सी० टावर की व्यवस्था कर ली गई थी।
यदि पुराने इतिहास पर दृष्टि डालकर देखा जाए तो पता चलेगा कि यह समुद्री तूफान व बाढ़ कोई नई घटना नहीं है। प्राचीन इराक में आज से लगभग छह हजार वर्ष पूर्व आए समुद्री तूफान और बाढ़ से हुई तबाही के प्रमाण मिलते हैं। बाइबल और कुरान शरीफ में भी विनाशकारी तूफानों का वर्णन मिलता है। श्रीमद्भागवद्पुराण’ में भी प्रलय का उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि जब प्रलय से सृष्टि का विनाश हो रहा था तब मनु भगवान् ने एक नौका पर सवार होकर सभी प्राणियों के एक-एक जोड़े को बचा लिया था। भले ही यह वर्णन कथा के रूप में कहा गया है, किंतु इससे यह सिद्ध होता है कि समुद्र में तूफान आदिकाल से आते रहे हैं जिनका सामना मनुष्य करता आया है। इतना ही नहीं, भूकंप और समुद्री तूफानों ने पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन भी कर दिए हैं। इन्हीं ने नए द्वीपों व टापुओं की रचना भी की है।
भारत में प्राचीन द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। इसके आज भी प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक विश्व के अन्य स्थानों की परिवर्तित स्थिति का कारण समुद्री तूफानों व भूकंपों को मानते हैं। यू०एस० जियोलॉजिकल सर्वे के विशेषज्ञ केन हडनर के अनुसार सुमात्रा द्वीप से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में समुद्र-तल के नीचे आए, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 के लगभग थी। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने कई छोटे-बड़े द्वीपों को 20-20 मीटर तक अपने स्थान से हिलाकर रख दिया। विद्वानों का यह भी मत है कि यदि भारत अथवा एशिया के क्षेत्र में कहीं भी महासागर की तलहटी में होने वाली भूगर्भीय हलचलों के आकलन की चेतावनी प्रणाली विकसित होती तो इस त्रासदी से होने वाली जान-माल की क्षति को कम किया जा सकता था।
यह बात भी सही है कि प्राकृतिक प्रकोपों को रोक पाना मनुष्य व उसके साधनों के वश में नहीं है, फिर भी यथासंभव सूचना देकर बचने की कुछ व्यवस्था की जा सकती है। 26 दिसंबर, 2004 को सुनामी समुद्री भूकंप भारतीयों के लिए एक नया अनुभव है। भारतीय मौसम विभाग के सामने अन्य महासागरों में उठी सुनामी लहरों से हुई जान-माल की हानि के उदाहरण थे। किंतु भारतीय मौसम विभाग समुद्री भूकंप की सूचना होते हुए भी यह कल्पना तक नहीं कर सका कि सुनामी तरंगों से भारतीय तटीय क्षेत्र की दशा कैसी हो सकती है।
भारत में सुनामी तूफान से हुए विनाश को देखकर विश्वभर के लोगों के हृदय दहल उठे थे। अतः उस समय हम सबका कर्तव्य है कि हम तन, मन और धन से ध्वस्त लोगों के परिवार के साथ खड़े होकर उनकी सहायता करें। इसमें संदेह नहीं कि विश्व के अनेक देशों व संस्थाओं ने सुनामी से पीड़ित लोगों की धन से सहायता की है, किंतु इससे उनके अपनों के जाने का गम तो दूर नहीं किया जा सकता। हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनका धैर्य बँधाना चाहिए।

54. व्यायाम का महत्त्व
संकेत : भूमिका, व्यायाम की आवश्यकता, व्यायाम के लाभ, व्यायाम के प्रकार, व्यायाम और खेल-कूद, व्यायाम और योगाभ्यास, उपसंहार।
एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का पूर्ण आनन्द ले सकता है। अगर आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन की सभी प्रकार की सुविधाएँ उसके लिए व्यर्थ हैं। कालिदास ने भी अपने महाकाव्य ‘कुमारसम्भव’ में कहा है-“शरीरमाचं खलु धर्म साधनम्” ।
अर्थात् शरीर ही धर्म का मुख्य साधन है। स्वास्थ्य ही जीवन है और अस्वास्थ्य मृत्यु है। अस्वस्थ व्यक्ति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। बढ़िया-से-बढ़िया भोजन भी उसे विष के समान लगता है। यही नहीं, उसमें किसी भी काम को करने की क्षमता भी नहीं होती। यद्यपि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वास्थ्य-रक्षा के लिए व्यायाम की सर्वाधिक आवश्यकता है। व्यायाम से बढ़कर और कोई अच्छी औषधि नहीं है।
मानव-शरीर पाँच तत्त्वों से मिलकर बना है। यही पाँच तत्त्व मानव-शरीर के लिए आवश्यक हैं। जब इनमें से किसी तत्त्व की कमी होती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अतः शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम नितान्त आवश्यक है। अंग्रेज़ी की उक्ति भी है-‘A sound mind dwells in sound body.+ अर्थात् स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता रहता है तो उसका शरीर निरोग रहता है। जो लोग व्यायाम नहीं करते उनका पेट बढ़ जाता है अथवा गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है या रक्तचाप में विकार आ जाता है।
इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यायाम स्वास्थ्य-रक्षा का साधन है, परन्तु व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। जो लोग कुछ देर व्यायाम करके पुनः त्याग देते हैं उनको लाभ की बजाए हानि ही होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यायाम आयु और शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए।
व्यायाम से शरीर बलिष्ठ और सुडौल होता है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। यही नहीं, वह उद्यमी भी होता है। प्रतिदिन व्यायाम करने से खूब भूख लगती है और पाचन-शक्ति भी बढ़ती है। शरीर में रक्त का संचरण सही होता है। शरीर के माँस-पिण्ड और हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं। इसके विपरीत, जो लोग व्यायाम नहीं करते उनका शरीर रोगी हो जाता है। वे अक्सर डॉक्टरों और हकीमों के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। व्यायाम न करने वालों का शरीर दुबला-पतला रहता है।
व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। कुछ लोग व्यायाम का अर्थ दण्ड-बैठक लगाना ही लेते हैं, परन्तु शारीरिक व्यायाम में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनसे शरीर के अंग पुष्ट होते हैं। प्रातःकाल में खुली हवा में दौड़ लगाना या जोगिंग करना भी व्यायाम है। इसी प्रकार से कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर खुली हवा में सपाटे भरना पसन्द करते हैं। कुछ लोग नदी में तैरते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि नदी में तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है। इसी प्रकार से अखाड़े में कुश्ती करना या मुग्दर घुमाना भी व्यायाम है। कुछ लोगों का विचार है कि खेल-कूद में भाग लेने से ही स्वास्थ्य ठीक रहता है।
व्यायाम का सबसे अच्छा साधन खेल-कूद है। फुटबाल, वॉलीबाल, बास्कट बाल, खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिण्टन, जिमनास्टिक आदि असंख्य ऐसे खेल हैं जो व्यायाम के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप में किसी-न-किसी खेल में भाग लेता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए तो स्कूलों और कॉलेजों में खेल-कूद की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। खेलों के महत्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने एक खेल मन्त्रालय का भी गठन किया है। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष सभी प्रकार के खेलों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। एक स्वस्थ एवं विकसित राष्ट्र खेल-कूद तथा व्यायाम पर निर्भर करता है। इसीलिए स्कूलों तथा कॉलेजों में ‘शारीरिक विज्ञान’ की शिक्षा भी दी जा रही है।
व्यायाम का एक अन्य अच्छा और सस्ता साधन है-योगाभ्यास। इसमें कोई अधिक खर्च नहीं आता। घर में किसी स्थान पर पाँच-सात आसन अगर नियमित रूप से किए जाएं तो शरीर काफी स्वस्थ रहता है। उदाहरण के रूप में, प्राणायाम, पद्मासन, सर्वांगासन, गोमुख आसन, शवासन, सूर्य नमस्कार आदि कुछ ऐसे आसन हैं जिनके द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, परन्तु इन आसनों को किसी शिक्षक से सीखने के बाद ही करना चाहिए, तभी लाभ होगा नहीं तो हानि भी हो सकती है। योगाभ्यास को विद्यालयों में एक विषय के रूप में पढ़ाया भी जाता है। व्यायाम का सर्वाधिक अनुकूल समय प्रातःकाल है। इस समय वायु शुद्ध और स्वच्छ होती है। व्यायाम करने के बाद पौष्टिक और सात्विक भोजन करना चाहिए। बूढ़ों और रोगियों के लिए प्रातः और सायं का भ्रमण ही उचित है।
स्वास्थ्य ही मनुष्य का सच्चा धन है। अतः उसे बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा तीनों ही स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। युवक-युवतियों को प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। परन्तु अधिक व्यायाम करने से लाभ की बजाए हानि होती है। अतः उचित मात्रा में ही व्यायाम करना चाहिए। अच्छा तो यह है कि हम किसी योग्य शिक्षक की देख-रेख में ही व्यायाम करें। इसके लिए आजकल स्थान-स्थान पर व्यायाम केन्द्र खुल गए हैं।
55. शिक्षा में खेल-कूद का महत्त्व
संकेत : खेल-कूद का महत्त्व, शिक्षा व खेल-एक-दूसरे के पूरक, खेलों के प्रकार, लाभ, सर्वांगीण विकास। . ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा है-
“स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही भली प्रकार अपने
मस्तिष्क का विकास कर सकता है।”
शिक्षा का अभिप्राय केवल पुस्तकों का ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, अपितु शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक विकास के साथ-साथ उसके शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल-कूद का महत्त्व किसी से कम नहीं। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का। ईश्वर ने मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक-तीन शक्तियाँ प्रदान की हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन तीनों का संतुलित रूप से विकास होना आवश्यक है।
शिक्षा तथा खेल एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अपंग है। शिक्षा यदि परिश्रम लगन, संयम, धैर्य तथा भाईचारे का उपदेश देती है तो खेल के मैदान में विद्यार्थी इन गुणों को वास्तविक रूप में अपनाता है। जैसे कहा भी गया है- ‘स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
यदि व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो संसार के सभी सुख तथा भोग-विलास बेकार हैं। एक स्वस्थ शरीर ही सभी सुखों का भोग कर सकता है। रोगी व्यक्ति सदा उदास तथा अशांत रहता है। उसे कोई भी कार्य करने में आनंद प्राप्त नहीं होता है। स्वस्थ व्यक्ति सभी कार्य प्रसन्नचित्त होकर करता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर एक नियामत है। – खेलना बच्चों के स्वभाव में होता है। आज की शिक्षा-प्रणाली में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को पुस्तकों की अपेक्षा खेलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाई जाएँ। आज शिक्षा-विदों ने खेलों को शिक्षा का विषय बना दिया है, ताकि विद्यार्थी खेल-खेल में ही जीवन के सभी मूल्यों को सीख जाएं और अपने जीवन में अपनाएँ।
अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के खेलों का सहारा लिया जा सकता है। दौड़ना, कूदना, कबड्डी, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जिमनास्टिक, योगाभ्यास आदि से उत्तम व्यायाम होता है। इनमें से कुछ आउटडोर होते हैं और कुछ इंडोर। आउटडोर खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं। इंडोर खेलों को घर के अंदर भी खेला जा सकता है। इनमें कैरम, शतरंज, टेबलटेनिस आदि हैं। न केवल अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी खेलों का आयोजन होता रहता है। खेलों से न केवल खिलाड़ियों का अपितु देखने वालों का भी भरपूर मनोरंजन होता है। आज रेडियो तथा टी०वी० आदि माध्यमों के विकास से हम आँखों देखा हाल अथवा सीधा प्रसारण देख सकते हैं तथा उभरते खिलाड़ी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।
आज के युग में खेल न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि इनका सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व भी है। इनमें स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ-साथ मनोरंजन भी होता है। इनसे छात्रों में अनुशासन की भावना आती है। खेल के मैदान में छात्रों को नियमों में बंधकर खेलना पड़ता है, जिससे आपसी सहयोग और मेल-जोल की भावना का भी विकास होता है। खेल-कूद मनुष्य में साहस और उत्साह की भावना पैदा करते हैं। विजय तथा पराजय दोनों स्थितियों को खिलाड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। खेल-कूद से शरीर में स्फूर्ति आती है, बुद्धि का विकास होता है तथा रक्त संचार बढ़ता है। खेलों में भाग लेने से आपसी मन-मुटाव समाप्त हो जाता है तथा खेल भावना का विकास होना है। जीविका-अर्जन में भी खेलों का बहुत महत्त्व है।
आज खेलों में ऊँचा स्थान प्राप्त खिलाड़ी संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते हैं। किसी भी खेल में मान्यता प्राप्त खिलाड़ी को ऊँचे पद पर आसीन कर दिया जाता है तथा उसे सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। खेल राष्ट्रीय एकता की भावना को भी विकसित करते हैं। राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं।
भारत जैसे विकासशील देश के लिए आवश्यकता है कि प्रत्येक युवक-युवती खेलों में भाग ले तथा श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करे। आज का युग प्रतियोगिता का युग है और इसी दौड़ में किताबी कीड़ा बनना पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वस्थ, सफल तथा उन्नत व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक है मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक विकास।

56. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’
संकेत : भूमिका, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा, चुनौतीपूर्ण परवरिश, बेटी की सुरक्षा के लिए प्रयत्न, उपसंहार।
21 वीं सदी में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे की अनुगूंज चारों ओर सुनाई पड़ने लगी। इस नारे की क्या आवश्यकता है जब भारतवर्ष में प्राचीनकाल से नारी की स्तुति ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ कहकर की जाती रही है। यहाँ तक कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी देवताओं को नारी की शरण में जाना पड़ा था। देवी दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी महालक्ष्मी और दुष्टों का नाश करने वाली महाकाली की आराधना आज भी की जाती है। इतना ही नहीं, आधुनिक काल में आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने पर्दा प्रथा को त्यागकर देश को स्वतंत्रता दिलवाने में बढ़-चढ़कर भाग लिया।
कविवर पंत ने नारी को ‘देवी माँ’, ‘सहचरी’, ‘सखी’, ‘प्राण’ तक कहकर सम्बोधित किया है। आज नारी चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक विराजमान है। पुलिस, सुरक्षा बल व सेना तक में भी उच्च पदों पर नियुक्त है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ उसने अपनी प्रबल कर्मठता का परिचय नहीं दिया। वह हर पद पर पुरुषों से अधिक ईमानदारी से काम करती है, यह सत्य भी किसी से छिपा नहीं है। वह माँ बनकर सृष्टि की रचना करने जैसा पवित्र काम करती है। पत्नी और बहन बनकर अपने सामाजिक दायित्व को निभाती है। आज अपने महान सहयोग से देश के विकास में बराबर की सहभागी बन गई है। फिर उसे हीन-भाव से क्यों देखा जाता है। वे कौन-से कारण हैं जिनके रहते बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आज इन कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है।
यदि ध्यान से देखा जाए तो आजकल माता-पिता के लिए बेटी की परवरिश करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि यौन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। माता-पिता की सोच बनती जा रही है कि यदि हम बेटी की इज्जत की रक्षा न कर पाए तो बेटी को जन्म देने का क्या फायदा होगा। माता-पिता की यही सोच कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण है। इसके साथ-साथ दहेज प्रथा के कारण भी लोग बेटी को आर्थिक बोझ समझते हैं। बेटी का बाप बनना अच्छा नहीं समझा जाता है। बेटे वंश चलाते हैं, बेटी नहीं। आज यौन-अपराध व बलात्कार की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त बेटी को पराया धन कहकर उसकी तौहीन की जाती है। इन सभी कारणों से बेटी को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। यदि समस्या की गहराई में झांका जाए तो इसमें बेटी कहाँ दोषी है ? दोषी तो समाज या उसकी संकीर्ण सोच है। आज बेटियों की कमी के कारण अनेक नई-नई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। स्त्री-पुरुष संख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि बेटियाँ नहीं होंगी तो बहुएँ कहाँ से आएंगी। आज आवश्यकता है, बेटियों को बेटों के समान समझने की। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की। समाज के अपराध बोध को दूर करने की। दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या अपनी कब्र खोदने के समान है।
‘इनकी आहों को रोक न पाएंगे हम
अपने किए पर पछताएंगे हम।’ इस दिशा में सरकार ने अब अनेक कदम उठाएँ हैं ताकि बेटियों को बचाया जा सके और जिन कारणों से बेटियों को बोझ समझकर जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, उन्हें दूर किया जा सके। सरकार की इन योजनाओं में ‘बेटी धन’ योजना प्रमुख है। इसमें बेटी की शिक्षा व विवाह में आर्थिक सहायता की जाती है।
‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे के दूसरे भाग ‘बेटी पढ़ाओ’ पर भी विचार करना जरूरी है। ‘बेटी पढ़ाओ’ का सम्बन्ध नारी-शिक्षा से है। नारी हो या पुरुष शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है किन्तु बेटी-जीवन के सम्बन्ध में शिक्षा का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यदि बेटी शिक्षित होकर स्वावलम्बी बन जाती है तो वह माता-पिता पर बोझ न बनकर उनका बेटों के समान सहारा बन सकती है। बेटी बड़ी होकर देश की भावी पीढ़ी को योग्य बनाने के कार्य में उचित मार्ग-दर्शन कर सकती है।
बच्चे सबसे अधिक माताओं के सम्पर्क में रहते हैं। माता के व्यवहार का प्रभाव बच्चों के मन पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसी स्थिति में बेटियों का पढ़ना अति-आवश्यक है। आज की शिक्षित बेटी कल की शिक्षित माँ होगी जो देश और समाज के उत्थान में सहायक बन सकती है। इसीलिए बेटियों का सुशिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित व्यक्ति ही अपना हित-अहित, लाभ-हानि भली-भाँति समझ सकता है। शिक्षित बेटियाँ ही अपने विकसित मन-मस्तिष्क से घर की व्यवस्था सुचारु रूप से चला सकती हैं तथा घर-परिवार के लिए आर्थिक उपार्जन भी कर सकती हैं। बेटियाँ पढ़-लिखकर योग्य बनकर आधुनिक देश-काल के अनुरूप उचित धारणाओं, संस्कारों और प्रथाओं का विकास करके कुप्रथाओं व कुरीतियों को मिटाकर एक स्वस्थ एवं उन्नत समाज का निर्माण कर सकती हैं। बेटी पढ़ाओ की दिशा में आज समाज, देश व सरकार प्रयत्नशील हैं।
आज बेटी बचाने की आवश्यकता के साथ-साथ बेटियों को शिक्षित, विवेकी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनाने की भी आवश्यकता है। इसी से बेटियों व नारियों संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान सम्भव है। तभी, वे बराबरी और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगी। तब बेटी बचाओ जैसे नारों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

57. आधुनिक नारी
अथवा
नारी और नौकरी
संकेत : नारी का समाज में महत्त्व, मध्यकाल में दशा, आधुनिक नारी, हर क्षेत्र में आगे, समस्याएँ, ममता की देवी।
जिस प्रकार तार के बिना सितार तथा धुरी के बिना पहिया बेकार होता है; उसी प्रकार नारी के बिना नर का जीवन चल नहीं सकता। गृहस्थी की गाड़ी नर तथा नारी दोनों के सहयोग से आगे बढ़ती है। गृहस्थी का कोई भी कार्य नारी के बिना संभव नहीं है। वैदिक काल में नारियों को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मनु महाराज ने नारी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए यह घोषणा की
‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।’
अर्थात् जिस घर में नारी का आदर और सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। उस समय हर धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। स्त्रियों को अपना वर चुनने का अधिकार था। नारी को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त थे। वे शिक्षा प्राप्त करती थीं। वे पति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती थीं और शास्त्रार्थ करती थीं। इस प्रकार प्राचीन काल में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी।
मध्यकाल तक आते-आते नारी की स्थिति दयनीय हो गई थी। भारत पर मुसलमानों का राज्य हो गया। उनकी सभ्यता ने हिंदू समाज को प्रभावित किया। नारी की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया। वह घर की चारदीवारी में बंद कर दी गई। बाल-विवाह और सती प्रथा का प्रचलन बढ़ा। अशिक्षित होने के कारण नारी ने इसे अपना भाग्य मान लिया। मैथिलीशरण गुप्त ने उस समय की नारी की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए लिखा है
‘अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।’
आधुनिक युग में अनेक समाज-सुधारकों-राजा राम मोहनराय, महर्षि दयानंद आदि ने नारी-उद्धार के लिए प्रयत्न किए। उन्हें समान अधिकार दिलवाने के लिए कोशिश की। भारत का स्वतंत्रता-संग्राम तो मानो नारी-मुक्ति का संदेश लेकर आया। स्वतंत्र भारत के संविधान में नारी को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त हुए तथा नागरिकों के कर्त्तव्य में प्रमुख कर्त्तव्य था-नारी जाति का सम्मान करना।
आज भारतीय नारी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वे पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। वे पुरुष के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आज नारी अध्यापिका, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, राजदूत, गवर्नर, प्रधानमंत्री, पायलट, ट्रक-ड्राइवर तथा रेलगाड़ी ड्राइवर है तथा खेलों में भी भाग ले रही है। आज नारी ने अपने व्यक्तित्व को पहचान लिया है। नौकरी करने से जहाँ एक ओर उसमें आत्म-विश्वास पैदा हुआ है; वहीं दूसरी ओर उसने अपने घर व परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा है। कहा जाता है कि यदि लड़का पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है और यदि लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक शिक्षित नारी न केवल अपने परिवार के स्तर को ऊँचा उठाती है, बल्कि वह समाज के प्रति भी सजग होती है। वह वर्तमान समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती है तथा समाज-सुधार के कार्य करती है। भारतीय नारी ने शिक्षित तथा आधुनिक बनकर भी नम्रता, लज्जा तथा मर्यादा आदि गुणों को नहीं त्यागा।
आधुनिक युग में जहाँ नारी को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वहीं उसे पग-पग पर अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उसके उत्तरदायित्वों में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। घर के सभी काम करने के बाद वह घर से बाहर नौकरी भी करती है। घर तथा नौकरी की जिम्मेदारियों के नीचे वह पिस रही है। पुरुष के सहयोग के बिना मशीन की भाँति काम करते हुए उसमें मानसिक द्वंद्व पैदा होता है। उसमें नीरसता बढ़ती जा रही है। कई बार वह मातृत्व का दायित्व भी कुशलतापूर्वक निभा नहीं पाती। परंतु आधुनिक नारी इन सब समस्याओं पर विजय पाने का प्रयास कर रही है। आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होने पर वह आत्म-विश्वास के साथ समस्याओं का सामना करती है, पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती, अपने जीवन को भार नहीं समझती और निराश होकर आत्महत्या की ओर नहीं दौड़ती।
खुशी की बात है कि हमारी सरकार इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है। काम और वेतन की समानता के सम्बन्ध में हमारे संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं। धीरे-धीरे स्त्रियाँ पर्दे की कैद से बाहर निकल रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बैंकों तथा अन्य कार्यालयों में स्त्रियाँ काम करने लगी हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में पुरुषों को भी उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए उपयोगी साहित्य तैयार किया जाए ताकि नारी को समाज में वही दर्जा मिले जो प्राचीन काल में सीता, अनुसूया, मैत्रेयी आदि स्त्रियों को प्राप्त था, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है।
आधुनिक नारी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रही है। पश्चिमी नारी का अंधानुकरण करते हुए वह परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों तथा आदर्शों को भूल रही है। वह सादगी तथा सरलता को त्याग कर फैशन तथा आडंबरपूर्ण जीवन को अपना रही है। पैसा कमाने की होड़ में वह नैतिक मूल्यों को खो चुकी है। नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र तथा सुरक्षित हो, शिक्षित और आत्म-विश्वासी हो, परंतु स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे। उसे अपने स्वाभाविक गुणों सरलता, विनम्रता, ममता, त्याग आदि को त्यागना नहीं है। उसे सभी का सुख चाहने वाली, त्यागमयी, ममता की देवी बनना है। ऐसी शक्ति मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। जयशंकर प्रसाद ने नारी के इसी रूप का वर्णन करते हुए कहा है-
नारी! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग, पद, तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।
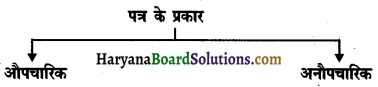
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()