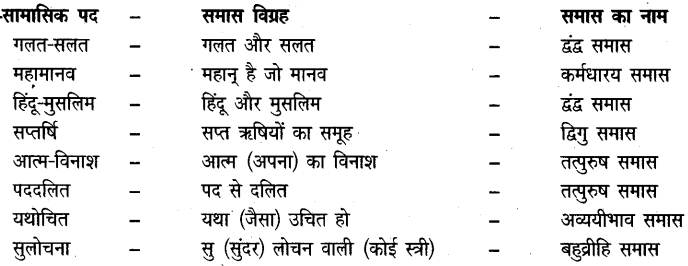HBSE 10th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 4 एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!
Haryana State Board HBSE 10th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 4 एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा! Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 10th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 4 एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!
HBSE 10th Class Hindi एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा! Textbook Questions and Answers
एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा Question Answer HBSE 10th Class प्रश्न 1.
हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है?
उत्तर-
प्रस्तुत कहानी में लेखक ने उपेक्षित समाज के लोगों द्वारा आज़ादी की लड़ाई में योगदान पर प्रकाश डाला है। दुलारी एक गीत गाने वाली स्त्री है, जिसे समाज हेय दृष्टि से देखता है। टुन्नू एक किशोर युवक है। वह भी गीत गाता है तथा राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेता है। दुलारी को फेंकू सरदार मानचेस्टर तथा लंका शायर की मिलों में बनी मखमली किनारे वाली कोरी धोतियों का बंडल लाकर देता है। दुलारी को बढ़िया-बढ़िया साड़ियाँ पहनने का चाव भी है। किंतु दुलारी के मन में देश-प्रेम की भावना भी है। वह उस बंडल को विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर उनकी होली जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को दे देती है। वह टुन्नू के द्वारा दी हुई खादी आश्रम में बनाई साड़ी को पहनती है। वह फेंकू सरदार, जो अंग्रेज़ों का मुखबर है, को झाड़ मार-मार कर घर से निकाल देती है। टुन्नू विदेशी वस्त्रों को जला देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देता है और इसी कारण अंग्रेज़ पुलिस द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार लेखक ने प्रस्तुत कहानी में समाज में उपेक्षित समझे जाने वाले लोगों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए सहयोग का सजीव चित्रण किया है।
![]()
Class 10th Kritika Chapter 4 Question Answer HBSE प्रश्न 2.
कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी?
उत्तर-
दुलारी एक गौनहारी है। उसे अत्यंत कठोर हृदय वाली स्त्री समझा जाता है। होली के अवसर पर साड़ी लाने पर वह टुन्नू को डाँट देती है। इतना ही नहीं, वह साड़ी को फैंक देती है। किंतु जब टुन्नू उसे कहता है कि “मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उमर का कायल नहीं होता।” उसके ये शब्द सुनकर कठोर दिखने वाली दुलारी का मन ही नहीं, आत्मा भी पिघल जाती है। टुन्नू के चले जाने पर वह साड़ी को उठाकर बार-बार चूमती है। इसी प्रकार दुलारी जब टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुनती है तो व्याकुल हो उठती है और उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उसने जान लिया था कि टुन्नू उसके शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करता है। वह उसकी गायन कला का प्रेमी था। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर गौनहारिन दुलारी का विचलित होना स्वाभाविक था।
कक्षा 10 कृतिका पाठ 4 के प्रश्न उत्तर HBSE प्रश्न 3.
कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादो मास की तीज़ के अवसर पर गाया जाता है। कजली दंगल में दो कजली-गायकों के बीच प्रतियोगिता होती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन पर खूब भीड़ जमा होती थी। यह आम जनता के मनोरंजन का प्रमुख साधन भी था। मनोरंजन के लिए ही ऐसे दंगलों का आयोजन किया जाता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था तथा गायन शैली में नए प्रयोग भी किए जाते थे। स्वतंत्रता के आंदोलनों के समय तो इन दंगलों के माध्यम से जनता में देश-भक्ति की भावना का संचार किया जाता था। हरियाणा में रागनी प्रतियोगिता व सांग भी लोक नाट्य परंपरा के प्रमुख उदाहरण हैं। ‘आल्हा- उत्सव’ राजस्थान की लोक गायन कला है। आजकल क्षेत्रीय लोक-गायकी के आयोजन किए जाते हैं। लोक-गायक इनमें बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं।
Class 10th Hindi Kritika Chapter 4 Question Answer HBSE प्रश्न 4.
दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। -इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए।
उत्तर-
गौनहारिन होने के कारण दुलारी को समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। वह समाज की दृष्टि में उपेक्षित और तिरस्कृत है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक दायरे से बाहर है। किंतु उसके व्यक्तिगत गुण इतने अच्छे हैं कि वह अति विशिष्ट समझी जाती है। उसके अग्रलिखित गुण व व्यक्तिगत विशेषताएँ ही उसे यह दर्जा दिलवाते हैं
- कुशल गायिका-दुलारी एक कुशल गायिका थी। हर व्यक्ति उसके सामने गीत -गाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसका स्वर मधुर एवं आकर्षक था। वह मौके के अनुसार हर प्रकार का गीत गा सकती थी।
- कवयित्री-दुलारी एक कुशल गायिका ही नहीं, अपितु सफल कवयित्री भी थी। वह आशु कवयित्री थी। वह तुरंत ऐसा पद्य तैयार कर देती थी कि सुनने वाले दंग रह जाते थे।
- स्वाभिमानी-दुलारी को भले ही समाज उपेक्षा के भाव से देखता था, किंतु वह कभी किसी वस्तु के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। जब कभी उसके स्वाभिमान पर चोट की गई तो उसने अपने स्वाभिमान की स्वयं साहसपूर्वक रक्षा की।
- सच्ची प्रेमिका-दुलारी एक गौनहारिन है। उसे समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। किंतु उसके हृदय में सच्चे प्रेम के प्रति आदर का भाव है। वह टुन्नू के हृदय की भावना को समझ जाती है। वह उससे मन-ही-मन प्रेम करने लगती है। जब फेंकू सरदार टुन्नू के विषय में कुछ गलत कहता है, तो वह उसे झाड़ से पीटती हुई घर से बाहर निकाल देती है।
Chapter 4 Kritika Class 10 HBSE प्रश्न 5.
दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ?
उत्तर-
दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के अवसर पर आयोजित ‘कजली दंगल’ में हुआ था। इस कंजली दंगल का आयोजन खोजवाँ बाजार में हो रहा था। दुलारी खोजवाँ वालों की ओर से प्रतिद्वंद्वी थी, तो दूसरे पक्ष यानि बजरडीहा वालों ने टुन्नू को अपना प्रतिद्वंद्वी बनाया था। इसी प्रतियोगिता में दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय हुआ था।
![]()
Class 10th Kritika Chapter 4 HBSE प्रश्न 6.
दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था-“तें सरबउला बोल ज़िन्नगी में कब देखले लोट?…” दुलारी ‘ के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
दुलारी इस कथन के माध्यम से टुन्नू पर यह आक्षेप लगाती है कि वह बढ़-चढ़कर बोलता है। उसके कथनों में सत्यता नहीं है। इसी प्रसंग में आगे वह उस पर बगुला भगत होने का भी आक्षेप लगाती है। वह आज के युवा-वर्ग को बड़बोलापन त्यागकर गंभीर बनने का संदेश देती है। उन्हें आडंबरों को त्यागकर गाँधी जी जैसा सीधा-सादा जीवन जीना चाहिए। देश के लिए त्यागशीलता की भावना होना अनिवार्य है।
Class 10 Kritika Chapter 4 Question Answer HBSE प्रश्न 7.
भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया ?
उत्तर-
दुलारी और टुन्नू ने अपने-अपने ढंग से भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दिया। टुन्नू ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में भाग लेकर विदेशी शासकों का विरोध किया। उसने विदेशी वस्त्र इकट्ठे करके उनकी होली जलाई जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। इसी आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े।
दुलारी एक गौनहारिन थी, किंतु उसके हृदय में देशभक्ति की भावना भी विद्यमान थी। उसने फेंकू सरदार द्वारा दी गई कीमती साड़ियों को विदेशी वस्त्रों की होली में फेंक दिया और खादी की साड़ी धारण की। टुन्नू की निर्मम हत्या से वह व्याकुल हो उठी और उसके बलिदान पर आँसू बहाने लगी।
कक्षा 10 कृतिका पाठ 4 के प्रश्न-उत्तर HBSE प्रश्न 8.
दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है?
उत्तर-
कहानी से पता चलता है कि दुलारी और टुन्नू के बीच शारीरिक प्रेम नहीं था। उनका प्रेम आत्मिक प्रेम था। दुलारी के गायन और उसकी काव्य कला से टुन्नू बहुत प्रभावित था। टुन्नू अभी सोलह-सत्रह वर्ष का किशोर था और दुलारी यौवन की अंतिम सीमा भी लाँघने वाली थी। वह उसे फटकारती भी है कि मैं तुम्हारी माँ से भी एक-आध वर्ष बड़ी हूँ। उसके मन के किसी एकांत कोने में टुन्नू ने अपना स्थान बना लिया था। यह सब दोनों के कलाकार मन और कला के कारण ही हुआ। टुन्नू द्वारा विदेशी कपड़ों के स्थान पर खादी पहनना और देश के लिए मर-मिटना दुलारी को भी देश-प्रेम के बहाव में बहाकर ले जाता है। वह टुन्नू की कुर्बानी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपनी कीमती साड़ियों का बंडल अग्नि के हवाले कर दिया। स्वयं भी खादी की धोती पहनकर उस स्थान पर जाने के लिए तत्पर हो गई, जहाँ टुन्नू का कत्ल किया गया था। कहने का भाव है कि टुन्नू का महान् त्याग ही दुलारी को देश-प्रेम के मार्ग पर ले आता है।
Class 10 Kritika Chapter 4 HBSE प्रश्न 9.
जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे-पुराने थे परंत दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? ..
उत्तर-
विदेशी वस्त्रों को जलाने वाले आंदोलनकारियों द्वारा फैलाई गई चादर पर लोग फटे-पुराने वस्त्र ही फेंक रहे थे। अच्छे वस्त्र उनमें बहुत ही कम थे। किंतु दुलारी ने फेंकू सरदार द्वारा लाई गई विदेशी साड़ियों को ही आग के हवाले करने के लिए दे दिया था। इससे पता चलता है कि उसके मन में देश-प्रेम की सच्ची भावना थी।
एही ठैयाँ झुलनी हो रामा HBSE 10th Class प्रश्न 10.
“मन पर किसी का बस नहीं है; वह रूप या उमर का कायल नहीं होता।” टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? ?
उत्तर-
निश्चय ही टुन्नू का यह कथन सत्य है। मन पर किसी का बस नहीं चलता। वैसे भी टुन्नू का दुलारी के प्रति आत्मिक प्रेम था। उसे दुलारी के रूप व आयु से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि यह प्रेम शरीर की भूख की तृप्ति के लिए नहीं था। इसलिए उसने इसे देश-प्रेम के मार्ग की ओर मोड़ दिया था जो स्वार्थहीन और प्रेम का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च स्वरूप है। देश-प्रेम के रूप में व्यक्ति की आत्मा का उदात्तीकरण होता है। टुन्नू देश के लिए अपना बलिदान कर देता है। दुलारी में देश के प्रति सद्भावना जागती है। वह विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर खादी आश्रम में बनी सूती धोती धारण करती है और टुन्नू की मृत्यु पर बेचैन हो उठती है। कहने का भाव है कि दोनों का प्रेम देश-प्रेम में बदल गया था।
Class 10 Hindi Kritika Chapter 4 Question Answer HBSE प्रश्न 11.
‘एही छैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!’ का प्रतीकार्थ समझाइए।
उत्तर-
यह पंक्ति लोकगीत की प्रथम पंक्ति है। इसका शाब्दिक अर्थ है-इसी स्थान पर मेरी नाक की लोंग खो गई है। इसका प्रतीक अत्यंत गंभीर है। नाक में पहना जाने वाला झुलनी नामक आभूषण सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गौनहारिन है। वह किसके नाम की झुलनी अपने नाक में पहने। किंतु आत्मिक स्तर पर वह टुन्नू से प्रेम करती थी और उसी के नाम की झुलनी उसने मानसिक व आत्मिक स्तर पर पहन ली थी। जिस स्थान पर वह यह गीत गा रही थी, उसी स्थान पर टुन्नू की हत्या की गई थी। अतः इस पंक्ति का भावार्थ यह हुआ कि यही वह स्थान है जहाँ उसका सुहाग लुटा था।
![]()
HBSE 10th Class Hindi एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा! Important Questions and Answers
एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा HBSE 10th Class प्रश्न 1.
“एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!” पाठ का उद्देश्य/मूलभाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
इस पाठ में लेखक का परम उद्देश्य उपेक्षित कहे जाने वाले लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए महान् सहयोग को उजागर करना है। इस लक्ष्य में लेखक पूर्ण रूप से सफल रहा है। इस पाठ में लेखक ने टुन्नू और दुलारी के आत्मिक प्रेम को देश-प्रेम जैसी उदात्त भावना में परिवर्तित करके इस लक्ष्य की पूर्ति की है। टुन्नू किशोरावस्था में है और दुलारी यौवन के अंतिम छोर पर खड़ी है। टुन्नू का दुलारी के प्रति प्रेम आत्मिक प्रेम है। उसे उसके रूप-सौंदर्य से कुछ लेना-देना नहीं है। वह उसके कलाकार मन से प्रेम करता है। दुलारी भी उससे इसी भाव से प्रेम करती है। उसको फटकार कर उसका हित चाहती है। किंतु उसके जाने के बाद अपने मन में एक अजीब-सा भाव अनुभव करती है। टुन्नू के प्रति फेंकू सरदार द्वारा कहे गए अपशब्द सुनकर वह उसे झाड़ से पीटकर घर से बाहर निकाल देती है। फेंकू सरदार द्वारा दी गई कीमती साड़ियों को विदेशी वस्त्रों की होली में फैंक देती है और खादी की साड़ी धारण कर लेती है तथा टुन्नू की हत्या करने वालों पर व्यंग्य करती है। अतः इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य देश-प्रेम और त्याग की भावना की प्रेरणा देना है।
Hindi Class 10 Chapter 4 Kritika HBSE प्रश्न 2.
दुलारी के दिन का आरंभ कैसे होता था?
उत्तर-
दुलारी के दिन का आरंभ कसरत से होता था। वह मराठी महिलाओं की भाँति धोती तथा कच्छा-बाँधकर प्रतिदिन प्रातःकाल कसरत करती थी। वह इतनी कठोर कसरत करती थी कि उसके शरीर से पसीना बहने लगता था। कसरत करने के पश्चात् वह अंगोछे से अपना पसीना पोंछती थी। वह सिर पर बंधे बालों के जूड़े को खोलकर बालों को सुखाती थी। उसके पश्चात् वह आदम कद शीशे के सामने खड़ी होकर पहलवानों की भाँति अपने भुजदंडों को मुग्ध दृष्टि से देखती थी। उसका प्रातःकाल का नाश्ता प्याज, हरी मिर्च व भीगे हुए चनों से होता था।
प्रश्न 3.
पठित पाठ के आधार पर टुन्नू के चरित्र पर प्रकाश डालिए। अथवा [H.B.S.E. March, 2018 (Set-A)] टुन्नू के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
टुन्नू “एही छैयां झुलनी हेरानी हो रामा!” कहानी का प्रमुख पात्र है। उसे कहानी का नायक भी कहा जा सकता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं
- गायक-वह एक उच्चकोटि का गायक कलाकार है। वह एक किशोर है, किंतु अपनी गायिकी से सुप्रसिद्ध गौनहारिन दुलारी का मुकाबला ही नहीं करता, अपितु उसे मात भी दे देता है।
- गुण ग्राहक वह दूसरों के गुणों को शीघ्र ही पहचान लेता है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। जब उसे पता चलता है कि दुलारी महान् गायिका है तो वह श्रद्धापूर्वक उसके पास गायिकी सीखने के लिए जाता है। वह उसकी कला का पुजारी बन जाता है।
- देशभक्त निश्चय ही टुम्नू एक देशभक्त था। वह देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेता है और देश के लिए अपना बलिदान भी देता है।
- सच्चा प्रेमी-टुन्नू एक सच्चा प्रेमी है। वह दुलारी को एक कलाकार होने के नाते प्रेम करता है। उसका प्रेम आत्मिक है। इसलिए वह कहता भी है कि मन पर किसी का कोई बसें नहीं चलता। इससे सिद्ध हो जाता है कि उसके मन में दुलारी के प्रति सच्चा एवं पवित्र प्रेम भाव था।
प्रश्न 4.
दुलारी द्वारा टुन्नू के उपहार को ठुकराने के पीछे क्या भावना थी?
उत्तर-
दुलारी एक गौनहारिन स्त्री थी। वह नाच-गाकर लोगों का मन बहलाव करती थी। उसे समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। टुन्नू एक संस्कारी ब्राह्मण का पुत्र था। वह अभी किशोरावस्था में था। वह दुलारी की गायन कला से बेहद प्रभावित था। उसकी उम्र भी ऐसी न थी कि उसे समाज की ऊँच-नीच का पता हो। वह दुलारी के पास कभी-कभार आकर बैठ जाता था। उसने कभी कोई हल्की बात नहीं कही और न ही अपने मन की भावना ही प्रकट की। होली के त्योहार पर वह दुलारी को खादी की धोती उपहारस्वरूप देना चाहता था, किंतु दुलारी ने उसे फटकार दिया और उसके द्वारा लाई गई धोती को भी पटक दिया। दुलारी ने यह सब उसको अपमानित करने के लिए नहीं किया था। वह टुन्नू के प्रेम की सात्विकता की भावना को पहचानती थी। वह नहीं चाहती थी, टुन्नू उसकी बदनाम बस्ती में आए और समाज उसे और टुन्नू को लेकर ऊँगली उठाए। उसने टुन्नू के द्वारा लाए गए उपहार को इसलिए ठुकरा दिया था ताकि वह कभी उसकी ओर रुख न करे। वास्तव में वह टुन्नू की भलाई चाहती थी।
![]()
प्रश्न 5.
टुन्नू के पद्यात्मक आक्षेप का दुलारी ने क्या उत्तर दिया था?
उत्तर-
टुन्नू द्वारा दुलारी को साँवले रंग की और दूसरों द्वारा पोषित होने का आक्षेप लगाया गया था। इस आक्षेप को दुलारी ने हँसते-हँसते झेला और इसका उत्तर देती हुई वह गीत के माध्यम से कहती है, “अरे कोढ़ी अपने मुख पर लगाम दे, यहाँ तू बड़ी-बड़ी बातें बना रहा है। तेरा बाप तो घाट पर बैठा-बैठा सारा दिन कौड़ी-कौड़ी जोड़ता है। त सिर-फिरा है। तने कभी जिंदगी में नोट देखे भी हैं। कब देखे हैं, बता तू मुझसे परमेसरी नोट (वादा) माँग रहा है, जरा अपनी औकात तो देख।” इस प्रकार दुलारी ने टुन्नू की दयनीय आर्थिक दशा और अनुभवहीनता पर आक्षेप करके उसके आक्षेप का तगड़ा उत्तर दिया जिसे सुनकर सभा में उपस्थित लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की।
प्रश्न 6.
शर्मा जी द्वारा लिखित रिपोर्ट को सार रूप में लिखिए।
उत्तर-
शर्मा जी अखबार के रिपोर्टर थे। उन्होंने टुन्नू के कत्ल की घटना वाले दिन होने वाली वारदात पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसका सार इस प्रकार है
उन्होंने “एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!” शीर्षक रिपोर्ट में लिखा कि कल छह अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और जुलूस निकाला। इस जुलूस में टुन्नू ने भी भाग लिया था। जिसे पुलिस के जमादार अली सगीर ने पकड़ा और गालियाँ दीं। विरोध करने पर उसे ठोकर मारी। टुन्नू गिर पड़ा और उसके मुख से खून आने लगा। गोरे सिपाहियों ने उसे अस्पताल ले जाने का बहाना किया, किंतु उसे वरुणा के जल में प्रवाहित कर दिया। संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया था कि टुन्नू मर चुका था। टुन्नू और दुलारी के संबंधों की चर्चा करते हुए संवाददाता ने दुलारी को पुलिस के द्वारा बलपूर्वक टाऊन हॉल में उसी स्थान पर नाचने के लिए विवश करने का विवरण भी दिया जहाँ टुन्नू की हत्या की गई थी। वह नाचते हुए. आँखों से आँसू बहाती रही।
प्रश्न 7.
कजली दंगल की मजलिस के बदमज़ा होने का क्या कारण था? सार रूप में उत्तर दीजिए।
उत्तर-
खोजवाँ बाजार में कजली दंगल का आयोजन किया गया था। ‘कजली दंगल’ में दुलारी का मुकाबला टुन्नू कर रहा था। लोग दोनों के तेवर देखकर आनंद ले रहे थे। टुन्नू ने दुलारी पर कोयल की भांति दूसरों पर पोषित होने का आक्षेप किया, तो दुलारी ने भी उसे बगुला भक्त कहकर उसकी औकात की याद दिला दी। उसे बगुलाभक्त कहकर किसी बुरे नतीजे के लिए तैयार रहने के लिए चेताया। इस पर टुन्नू ने भी बढ़कर चोट करते हुए कहा कि तुम कितनी भी गालियाँ दो हम तो अपने मन की बात को डंके की चोट पर कहेंगे। इस बात पर फेंकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू को बचाया। इसके बाद कोई गाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मजलिस बदमज़ा हो गई।
प्रश्न 8.
‘एही छैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा, कासो मैं पूढूँ’-दुलारी के इस गीत का दूसरा चरण क्या है?
उत्तर-
‘सास से पूछू, ननदिया से पूछू, देवर से पूछत लजानी हो रामा’।
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
‘एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!’ शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है?
(A) शिवपूजन सहाय
(B) कमलेश्वर
(C) मधु कांकरिया .
(D) शिवप्रसाद मिश्र ‘रुद्र’
उत्तर-
(D) शिवप्रसाद मिश्र ‘रुद्र’
प्रश्न 2.
दुलारी ने किस प्रदेश की महिलाओं की भाँति धोती बाँधी हुई थी?
(A) महाराष्ट्र की महिलाओं की भाँति
(B) उत्तर प्रदेश की महिलाओं की भाँति
(C) हरियाणा की महिलाओं की भाँति
(D) पंजाब की महिलाओं की भाँति
उत्तर-
(A) महाराष्ट्र की महिलाओं की भाँति
![]()
प्रश्न 3.
पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है?
(A) सोते हुए
(B) गीत गाते हुए
(C) दंड लगाते हुए
(D) प्राणायाम करते हुए
उत्तर-
(C) दंड लगाते हुए
प्रश्न 4.
दुलारी को मिलने के लिए कौन आता है?
(A) दुलारी का भाई
(B) टुन्नू
(C) दुलारी का पिता
(D) पुलिस का सिपाही
उत्तर-
(B) टुन्नू
प्रश्न 5.
टुन्नू दुलारी के लिए क्या लेकर आया था?
(A) भोजन
(B) आभूषण
(C) खादी की साड़ी
(D) छाता
उत्तर-
(C) खादी की साड़ी
प्रश्न 6.
“मन पर किसी का बस नहीं। वह उमर या रूप का कायल नहीं।” ये शब्द किसने कहे हैं?
(A) दुलारी ने
(B) दुलारी की सखी ने
(C) किसी अजनबी ने
(D) टुन्नू ने
उत्तर-
(D) टुन्नू ने
प्रश्न 7.
दुलारी का मुख्य धंधा क्या था?
(A) काव्य रचना
(B) नृत्य करना
(C) कजली गीत गाना
(D) कीर्तन करना
उत्तर-
(C) कजली गीत गाना
प्रश्न 8.
‘तीर कमान होना’ का क्या अर्थ है?
(A) लड़ने के लिए तैयार होना
(B) तीर की भाँति तेज गति से जाना
(C) कमान की भाँति गोल होना..
(D) कमान से तीर चलाना
उत्तर-
(A) लड़ने के लिए तैयार होना
प्रश्न 9.
टुन्नू के पिता क्या कार्य करते थे?
(A) अध्यापन
(B) पंडिताई
(C) वकालत
(D) व्यापार
उत्तर-
(B) पंडिताई
प्रश्न 10.
दुलारी किस की ओर से कजली गाने आई थी?
(A) बजरडीहा की ओर से
(B) सुंदरगढ़ की ओर से
(C) खोजवाँ बाजार की ओर से
(D) राम नगर की ओर से
उत्तर-
(C) खोजवाँ बाजार की ओर से
![]()
एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा! Summary in Hindi
एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा! पाठ का सार
प्रश्न-
‘एही छैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा!’ शीर्षक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर-
प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यथार्थ और आदर्श, दंत कथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियों और उदात्तताओं को उजागर किया है। लेखक ने इन सबको क्षेत्रीय भाषा की रंगत में रंगकर अभिव्यक्त किया है। यह एक प्रेम कहानी-सी लगती है, किंतु इसमें प्रेम भाव के अतिरिक्त आदर्श, यथार्थ और व्यंग्य का संगम कुछ इस प्रकार हुआ है कि इन्हें अलग-अलग करके देखना संभव नहीं है। पाठ का सार इस प्रकार है
बनारस में चार-पाँच के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है-‘गौनहारिन परंपरा’ । कहानी की मुख्य नारी पात्र दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी रही है। दुलारी दनादन दंड लगा रही थी और उसका पसीना भूमि पर पसीने का पुतला बना रहा था। वह कसरत समाप्त कर पसीना पोंछ रही थी कि तभी किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने स्वयं को व्यवस्थित किया, धोती पहनी, केश बाँधे और दरवाज़ा खोल दिया। बगल में बंडल दबाए बाहर टुन्नू खड़ा था। टुन्नू भी एक गायक था। उसकी आँखों में शर्म और होंठों पर झेंप भरी मुस्कराहट थी। दुलारी ने आते ही उसे फटकरा, “ मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था न?” गिरे हुए मन से टुन्नू बोला, “साल भर का त्योहार था इसीलिए मैंने सोचा कि ……….,” कहते हुए उसने बगल से बंडल निकालकर दुलारी को दे दिया। इसमें खद्दर की एक साड़ी थी। दुलारी का रुख और कड़ा हो गया और बोली, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। तुम्हें जलने के लिए कोई और चिता नहीं मिली। तुम मेरे मालिक हो, बेटे हो, भाई हो क्या हो? उसने साड़ी टुन्नू के पैरों के पास फैंक दी। टुन्नू सिर झुकाए हुए ही बोला, “पत्थर की देवी भी अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती, फिर तुम तो हाड़-माँस की बनी हो। उसकी कज्जल भरी आँखों से आँसू टपक-टपककर धोती पर गिरने लगे। दुलारी कहती रही कि हाड़-माँस की बनी हूँ, तभी तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारे दूध के दाँत भी नहीं टूटे। बाप तो कौड़ी-कौड़ी जुटाकर गृहस्थी चलाता है और बेटा आशिकी के घोड़े पर सवार है। यह गली तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो शायद तुम्हारी माँ से भी वर्ष भर बड़ी हूँ।
पत्थर की तरह मूर्तिवत खड़ा टुन्नू बोला, ‘मन पर किसी का बस नहीं। वह उमर या रूप का कायल नहीं।’ वह धीरे-धीरे . सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसके जाने के बाद दुलारी के भाव बदले उसने धोती उठाई जिस पर टुन्नू के आँसू गिरे हुए थे। एक बार गली में टुन्नू को जाते देखा और धोती पर पड़े आँसुओं के धब्बों को बार-बार चूमने लगी।
भादो की तीज पर खोजवाँ बाजार में गाने का कार्यक्रम था। दुलारी गाने में निपुण थी। उसमें पद में सवाल – जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। बड़े-बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे। खोजवाँ बाजार वाले दुलारी को अपनी तरफ से खड़ा करके अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। उसके विपक्ष में सोलह-सत्रह वर्ष का टुन्नू किशोर था। टुन्नू के पिता यजमानी करके अपनी घर-गृहस्थी चलाते थे। किंतु टुन्नू को गायकी और शायरी का चस्का लग गया था। टुन्नू ने उस दिन जमकर दुलारी का मुकाबला किया। दुलारी को भी टुन्नू का गाना अच्छा लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के मुख से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के ‘मालिक’ फेंकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी का वार किया। दुलारी ने टुन्नू की उस वार से रक्षा की थी। टुन्नू के चले जाने के बाद भी दुलारी. उसी के विषय में सोचती रही। टुन्नू उस दिन अत्यंत सभ्य लग रहा था। दुलारी ने घर जाकर टुन्नू द्वारा दी हुई साड़ी को संदूक में रख दिया। उसके मन में भी टुन्नू के प्रति कोमल भाव जागृत होने लगे थे। टुन्नू कई दिनों से उसके पास आने लगा था और उसकी बातों को बड़े गौर से सुनने लगा था। दुलारी का यौवन ढल रहा था। टुन्नू सोलह-सत्रह वर्ष का था जबकि दुलारी दुनिया देख चुकी थी। वह समझ गई थी कि टुन्नू और उसका संबंध शारीरिक नहीं, आत्मा का था। वह यह बात टुन्नू के सामने स्वीकार करने से डर रही थी। उसी समय फेंकू धोतियों का एक बंडल लेकर उसके पास आता है। फेंकू सरदार उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वादा करता है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी गली में नीचे विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाली टोली निकली। लोग पुराने विदेशी कपड़े जलाने के लिए फैंक रहे थे। किंतु दुलारी ने फेंकू सरदार द्वारा दी गई बढ़िया साड़ियों का बंडल फैंक दिया। दुलारी द्वारा फैंके गए बंडल को देखकर सबकी आँखें उसकी ओर उठ गईं। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया।
दुलारी फेंकू सरदार की किसी बात पर बिगड़ गई और झाड़ से मारती हुई बोली निकल यहाँ से। यदि मेरी देहरी पर डाँका तो दाँत से तेरी नाक काट लूँगी। आँगन में खड़ी संगनियों और पड़ोसिनों ने दुलारी को अत्यंत हैरानी से देखा। चूल्हे पर चढ़ी दाल को दुलारी ने ठोकर मारकर गिरा दिया। दाल के गिरने से चूल्हे की आग तो बुझ गई, किंतु दुलारी के दिल की आग न बुझ सकी। पड़ोसिनों के मीठे वचनों की जलधारा से दुलारी के हृदय की आग कुछ ठंडी हुई। उनकी आपस की बातचीत से पता चला कि फेंकू सरदार टुन्नू से जलन रखता था। इसी बात को लेकर दुलारी ने फेंकू पर झाड़ बरसाए थे। तभी नौ वर्षीय झींगुर आकर बताता है कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश को उठा ले गए। टुन्नू की मौत की खबर सुनते ही दुलारी की आँखों से अश्रुधारा बह निकली। अब पड़ोसिनें दुलारी के दिल का हाल जान गई थीं। सभी ने उसके रोने को नाटक समझा किंतु दुलारी अपने मन की सच्चाई जानती थी। उसने टुन्नू द्वारा दी गई साधारण साड़ी पहन ली। वह झींगुर से टुन्नू की शहीदी के स्थान का पता पूछकर वहाँ जाने के लिए घर से निकली ही थी कि तभी थाने के मुंशी और फेंकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। न चाहते हुए भी उसे उनके साथ जाना पड़ा।
![]()
उधर अखबार के दफ्तर में प्रधान संवाददाता शर्मा जी की लिखी रिपोर्ट को पढ़कर क्रोध से लाल हो रहे थे। संपादक जी के आदेश पर शर्मा जी रिपोर्ट पढ़ने लगे, शीर्षक दिया था, “एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा,” रिपोर्ट में लिखा था कि कल नगर भर में हड़ताल थी। यहाँ तक कि खोमचे वाले भी बाजार में दिखाई नहीं दिए थे।
सुबह से ही विदेशी कपड़ों को एकत्रित करके उनकी होली जलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाऊन हॉल पर पहुंचकर समाप्त हो गया। जब सब अपने-अपने घरों को लौट रहे थे तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नूं को गालियाँ दीं। प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने खूब पीटा और बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली पर चोट आई। वह गिर पड़ा और उसके मुख से खून निकलने लगा। गोरे सिपाहियों ने उसे अस्पताल में ले जाने की अपेक्षा वरुणा में प्रवाहित कर दिया, जिसे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू नामक गायक का दुलारी से भी संबंध बताया जाता है।
शाम को टाऊन हॉल में आयोजित अमन सभा में जहाँ जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया व गवाया गया था। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहनी हुई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी, जहाँ आठ घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी उसने कुख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर गाया, किंतु उसके स्वर में दर्द स्पष्ट रूप में अनुभव किया जा सकता था। उसके गीत के बोल थे “एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा। कासों मैं पूछू।” उसने सारा गीत उस स्थान पर नज़र गड़ाकर गाया जहाँ टुन्नू का कत्ल किया गया था। गाते-गाते उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। उसके आसुओं की बूंदें ऐसी लग रही थीं जैसे टुन्नू की लाश को वरुणा के जल में फैंकने से उस जल की बूंदें छिटक गई थीं।” संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, किंतु इसे वे छाप न सके।
कठिन शब्दों के अर्थ
(पृष्ठ-31) दनादन = तेज़ गति से। चणक-चर्वण-पर्व = चने चबाने का त्योहार। बाकायदे = ठीक ढंग से। विलोल = असली। विलीन = गायब होना, नष्ट होना।
(पृष्ठ-33) शीर्ण वदन = कमज़ोर शरीर। खैरियत = कुशल। उपेक्षापूर्ण = निरादर के भाव से। कज्जल-मलिन = काजल से मैली हुई। पाषाण = पत्थर। प्रतिमा = मूर्ति। वक्र = टेढ़ी। दुक्कड़ = शहनाई के साथ बजाया जाने वाला यंत्र। महती = अत्यधिक। पद्य = कविता। क्षमता = शक्ति। कजली = एक प्रकार का लोकगीत। कायल = मानने वाला। कोर दबना = लिहाज करना।
(पृष्ठ-34) गौनहारियों की गोल = गाने वालों का समूह। प्रतिकूल = उलट। स्वर = आवाज़ । मुग्ध = मोहित। सार्वजनिक आविर्भाव = मंच पर लोगों के सामने अपनी कला दिखाने का अवसर। यजमानी = पुरोहित की जीविका। चस्का = स्वाद। रंग उतर गया = निराश हो गए। मद-विह्वल = अहंकार से पूर्ण। कोढ़ियल = कुरूप, कोढ़ के रोग से पीड़ित।
(पृष्ठ-35) सरबउला = पागल। व्यर्थ = बेकार। मजलिस = महफिल। बदमज़ा = बेस्वाद। प्रकृतिस्थ = स्वाभाविक। आबरवाँ = बहुत महीन मलमल। चंचल = अस्थिर, व्याकुल । दुर्बलता = कमज़ोरी।
(पृष्ठ-36) मनोयोग = लगन। यौवन का अस्ताचल = जवानी के समाप्त होने की दशा। उन्माद = पागलपन। कृशकाय = दुबला-पतला। पाँडुमुख = पीला मुख। करुणा = दया। आसक्त = मोहित, ललचाया हुआ। कृत्रिम = बनावटी। निभृत = एकांत। प्रस्तुत = तैयार। सहसा = एकाएक।
(पृष्ठ-37-38) आकृति = रूप, शक्ल । मुखबर = वह अपराधी जो अपराध स्वीकार करके सरकारी गवाह बन जाता है। तमोली = पान बेचने वाला। शपाशप = निरंतर। देहरी डाँकना = दहलीज पार करना। उत्कट = प्रबल। अधर = होंठ। कुतूहल = हैरानी। बटलोही = दाल पकाने का बर्तन। कातर = व्याकुल। स्तब्ध = हक्का-बक्का रह जाना। आँखों में मेघमाला घिर आना = आँखों से निरंतर आँसू बहना।
(पृष्ठ-39) कर्कशा = कटु वचन बोलने वाली। वनिता-सुलभ = सद् गृहिणियों के अनुरूप। दिल्लगी = मज़ाक। सहकर्मी = साथ काम करने वाला। बूते की बात नहीं = वश का काम नहीं। बड़ा घर = यहाँ जेल के लिए प्रयोग हुआ है। सजग = सावधान, चौकन्ने। झेंप = लज्जा। मुद्रा = भाव।
(पृष्ठ-40-41) विघटित = छंट गया, अलग-अलग हो गया। शव = मृत शरीर। विवश = मजबूर। आमोदित = प्रसन्न। उद्घांत दृष्टि = उड़ती-सी बेचैन नज़रें। अधर-प्रांत पर = होंठों पर। स्मित = हल्की-सी मुसकान। आविर्भाव = उदय होना।
HBSE 10th Class Hindi Solutions Kritika Chapter 4 एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा! Read More »