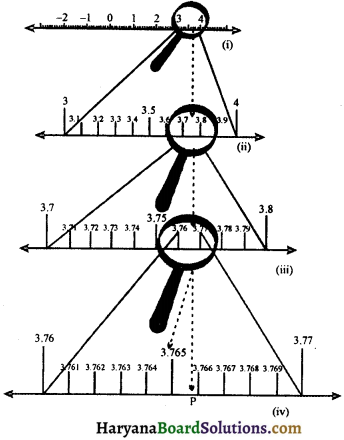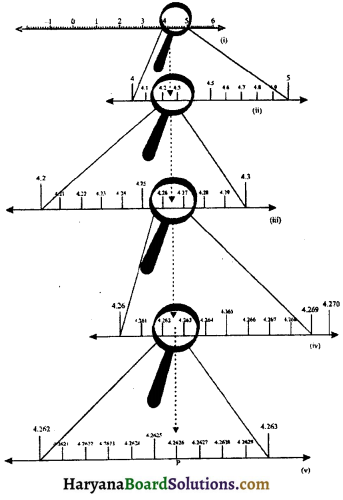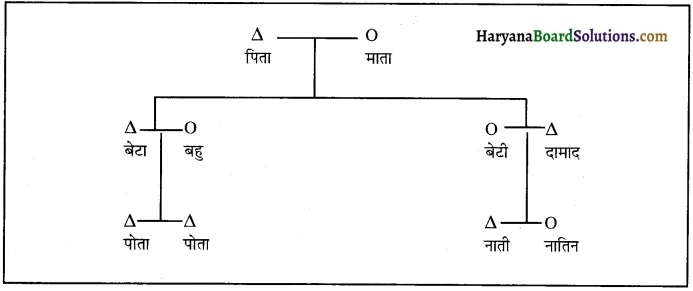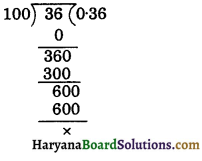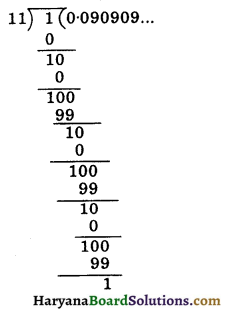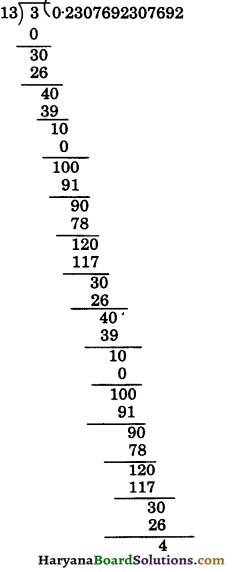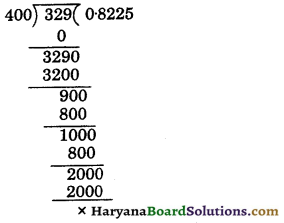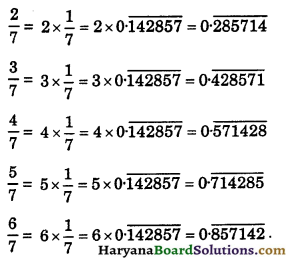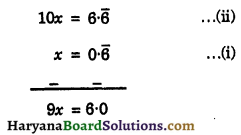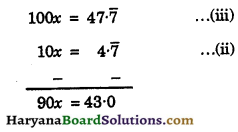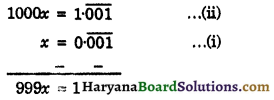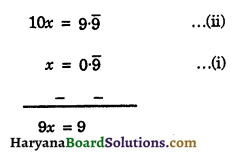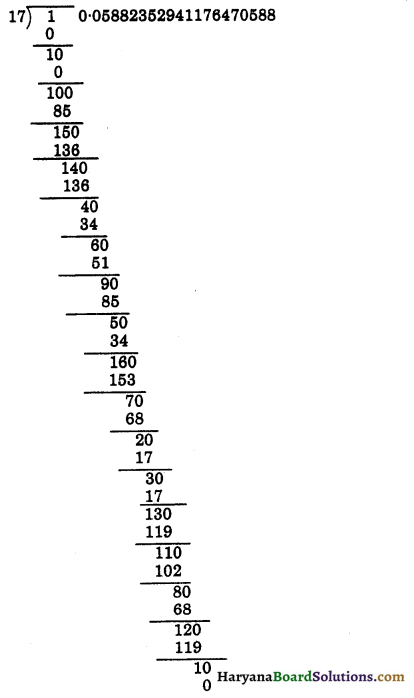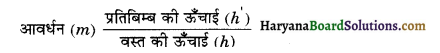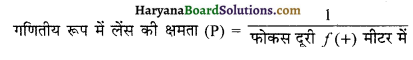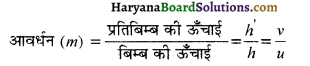Haryana State Board HBSE 12th Class English Solutions Flamingo Chapter 4 The Rattrap Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 12th Class English Solutions Flamingo Chapter 4 The Rattrap
HBSE 12th Class English The Rattrap Textbook Questions and Answers
Question 1.
How does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the ironmaster and his daughter? (फेरी वाले ने किसान, आयरन मास्टर एवं उसकी बेटी के द्वारा दर्शाए गए दयालुता एवं आतिथ्य के कार्यों का क्या अर्थ लिया ?)
Answer:
The peddler is a rattrap seller. He goes around selling small rattraps. But he does not earn enough to make both ends meet. So he resorts to begging as well as stealing to remain alive. He knocks at the door of an old crofter who welcomes him. He offers him food and shelter for the night. He plays a game of cards with him. But the rattrap seller steals his money. Then he seeks shelter in an old iron mill. The ironmaster mistakes him for his old friend. He and his daughter Edla persuade him to go with them and stay there on the Christmas eve.
They feed him well. The next morning, the servant bathes him, shaves him and gives him decent clothes to wear. But now the ironmaster realises his mistake. He discovers that the peddler is not his old friend. He asks him to go away. But his daughter Edla asks her father to let the peddler stay there for one more night. The poor peddler is moved by the love and affection shown by Edla. The love and affection shown by Edla awakens his essential goodness. Edla’s sympathy deeply moves him. Before going away, he leaves behind the money stolen from the crofter. He also leaves a rattrap as a gift for Edla.
(फेरी वाला चूहेदानियाँ बेचता है। वह छोटी-छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर जाता है। लेकिन वह इतना धन नहीं कमा पाता कि उसका गुजारा चल सके। इसलिए वह जिन्दा रहने के लिए भीख माँगने के साथ-साथ चोरी करने का भी सहारा लेता है। वह एक बूढ़े किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है जो कि उसका स्वागत करता है। वह उसे भोजन और रात बिताने के लिए आश्रय प्रदान करता है। वह उसके साथ ताश भी खेलता है। लेकिन चूहेदानियाँ बेचने वाला उसका धन चोरी कर लेता है। तब वह एक पुरानी लोहे की मिल में आश्रय लेता है।
आयरन मास्टर गलती से उसको अपना एक पुराना मित्र समझ लेता है। वह और उसकी बेटी एडला उस पर दबाव बनाते हैं कि वह उनके साथ चले और क्रिसमस की पूर्व संध्या उनके साथ बिताए। वे उसे अच्छी तरह से भोजन कराते हैं। अगली सुबह, नौकर उसे स्नान कराता है, उसकी दाढ़ी बनाता है और उसे पहनने के लिए सुन्दर कपड़े देता है। लेकिन तब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि फेरी वाला उसका पुराना मित्र नहीं है।
वह उसे चले जाने के लिए कहता है। लेकिन उसकी बेटी एडला अपने पिता से कहती है कि वह फेरी वाले को वहाँ पर एक और रात ठहरने की अनुमति दे दे। फेरी वाला एडला के द्वारा दर्शाए गए प्यार और स्नेह से बहुत प्रभावित हुआ। एडला द्वारा दर्शाए गए प्यार और स्नेह ने उसकी आंतरिक अच्छाई को जगा दिया। एडला की सहानुभूति ने उसको गहराई तक से प्रभावित कर दिया। जाने से पहले, वह किसान के यहाँ से चोरी किए धन को छोड़कर चला जाता है। वह एडला के लिए उपहारस्वरूप एक चूहेदानी भी छोड़कर जाता है।)
Question 2.
What are the instances in the story that show that the character of the ironmaster is different from that of his daughter in many ways?
(कहानी में वे उदाहरण कौन-से हैं जो दर्शाते हैं कि आयरन मास्टर का चरित्र कई प्रकार से उसकी बेटी से अलग है ?)or Edla is a better judge of character than her father. Justify. [H.B.S.E. 2019 (Set-B)] (एडला अपने पिता की तुलना में चरित्र में एक बेहतर न्यायधीश है। निरूपण करें।)
Answer:
There is a lot of difference between the character of the ironmaster and his daughter Edla. The ironmaster is the owner of the Ramsjö Ironworks. It is his ambition to produce good iron for the market. He is quite moody. When he sees the old peddler, he mistakes him as one of his old friends. He asks him, again and again, to come to his home for the night. When the peddler refuses, the ironmaster even brings his daughter to put pressure on him. But the next morning, when he realizes his mistake, he wants to hand over the peddler to the sheriff.
All his kindness and generosity vanish away. However, his daughter, Edla has all the qualities of head and heart. She has basic human qualities. She is kind, sympathetic and compassionate. She tells her father that it is wrong to chase away a man whom they themselves have invited to spend the night with them. She shows affection and sympathy to the peddler. The next morning, she is happy to find that the peddler is not a thief. Her goodness and compassion change the peddler’s heart. He leaves behind the old crofter’s money and also gives her a rattrap as a Christmas present.
(आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला के चरित्र में बहुत अधिक अंतर है। आयरन मास्टर रेमस्जो आयरन वर्क्स का मालिक है। उसका लक्ष्य बाजार के लिए उत्तम श्रेणी के लोहे का निर्माण करना है। वह पूरी तरह से अपनी मर्जी का मालिक है। जब वह बूढ़े फेरी वाले को देखता है तो वह उसे गलती से अपना एक पुराना मित्र मान लेता है। वह उसे बार-बार कहता है कि वह रात बिताने के लिए उसके घर चले। जब फेरी वाला मना कर देता है तो आयरन मास्टर उस पर दबाव बनाने के लिए अपनी बेटी को भी बुलाकर लाता है।
लेकिन अगली सुबह, जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह फेरी वाले को शेरिफ के हवाले करना चाहता है। उसकी सारी दयालुता और उदारता लुप्त हो जाती है। लेकिन उसकी बेटी एडला में सोच-विचार और दया के सारे गुण विद्यमान हैं। उसमें मानवता के आधारभूत गुण हैं। वह दयालु, सहानुभूतिपूर्ण एवं करुणामयी है। वह अपने पिता को बताती है कि उस आदमी को बाहर भगा देना एक गलत बात है जिस आदमी को अपने साथ रात बिताने के लिए उन्होंने स्वयं आमंत्रित किया था। वह फेरी वाले के प्रति स्नेह और सहानुभूति प्रकट करती है। अगली सुबह यह जानकर प्रसन्न होती है कि फेरी वाला कोई चोर नहीं है। उसकी अच्छाई और करुणा ने फेरी वाले के हृदय को परिवर्तित कर दिया। वह बूढ़े किसान वाले धन को वहीं छोड़ जाता है और एडला के लिए क्रिसमस के उपहारस्वरूप एक चूहेदानी छोड़ जाता है।)

Question 3.
The story has many instances of unexpected reactions from the characters to others’ behaviour. Pick out instances of these surprises.
(कहानी में पात्रों के अन्य लोगों के बर्ताव के प्रति अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कई उदाहरण हैं। ऐसे आश्चर्यों के उदाहरण ढूंढिए।)
Answer:
This story has a number of instances of unexpected reactions from the characters to others. One dark evening, the rattrap seller is going along a road. He is hungry and wants to spend the night somewhere. He sees a cottage by the roadside. He knocks at the door. He expects to meet some sour faces. But unexpectedly, an old man welcomes him cheerfully. He is an old crofter without wife or child. He serves him food, talks with him, and plays a game of cards with him till the bedtime. The next morning, the peddler steals his money and goes away. At night, he seeks shelter at an ironworks. Suddenly the master comes and behaves in an unexpected manner.
He mistakes him to be his old friend. He invites him to spend the night with him at his residence. When the peddler does not agree, he asks his daughter to persuade him. Finally, he goes with them. They offer him food and shelter for the night. The next morning, they ask the servant to bath and shave him. But then the ironmaster realises that the peddler is not his old friends. Now, he asks the peddler to go away at once. But his daughter Edla, unexpectedly, persuades her father to let him stay for the night. The peddler also behaves unexpectedly. The next morning, before going away, he leaves the stolen money and a rattrap as a present for Edla.
(इस कहानी में पात्रों के अन्य लोगों के व्यवहार के प्रति अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक अंधेरी शाम को चहेदानियाँ बेचने वाला सड़क पर अकेला जा रहा है। वह भूखा है और कहीं पर रात बिताना चाहता है। उसे सड़क किनारे एक घर दिखाई देता है। वह दरवाजा खटखटाता है। उसे उम्मीद है कि रूखा चेहरा ही उसका स्वागत करेगा। लेकिन उम्मीद के विपरीत एक बूढ़ा आदमी प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत करता है। वह एक बूढ़ा किसान है जो पत्नी अथवा बच्चे के बिना रहता है। वह उसे भोजन देता है, उसके साथ बातें करता है और रात को सोने के समय तक उसके साथ ताश खेलता है। अगली सुबह, फेरी वाला उसका धन चोरी कर लेता है और चला जाता है। रात के समय वह एक लोहे के कारखाने में आश्रय लेता है।
अचानक ही मालिक आता है और वह उसके साथ अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार करता है। वह गलती से उसे अपना एक पुराना मित्र समझ लेता है। वह उसे रात के समय अपने घर पर आने के लिए आमन्त्रित करता है। जब फेरी वाला सहमत नहीं होता है तो वह अपनी बेटी से कहता है कि वह उसे मनाए। अन्ततः वह उनके साथ जाता है। वे उसे रात के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। अगली सुबह, वे अपने नौकर से कहते हैं कि वह उसे स्नान कराए और उसकी दाढ़ी बनाए। लेकिन तब आयरन मास्टर को एहसास होता है कि फेरी वाला उसका पुराना मित्र नहीं है। तो वह फेरी वाले से वहाँ से तुरन्त चले जाने को कहता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी बेटी एडला अपने पिता पर दबाव बनाती है कि वह उसे रात के लिए वहीं ठहरने की अनुमति दे। फेरी वाला भी अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार करता है। अगली सुबह जाने से पहले वह चोरी किया गया धन और एडला के लिए उपहारस्वरूप एक चूहेदानी छोड़कर चला जाता है।)
Question 4.
What made the peddler finally change his ways? (फेरी वाले को अन्त में अपने तौर तरीके बदलने पर किस बात ने मजबूर किया ?)
Answer:
The peddler was a rattrap seller. But he could not earn enough money to make both ends meet. So he often committed petty thefts also. One night an old man gave him food and shelter for the night. He showed love and sympathy to him. But the peddler proved to be ungrateful man. Before going away, he steals the old man’s money. But in the end, he is a transformed man. His basic human qualities are awakened through the love and understanding shown to him by the ironmaster’s daughter, Edla. The ironmaster invites him to spend the night with him. His daughter Edla shows sympathy and compassion to him.
When the ironmaster realises his mistake, he asks him to go. But Edla persuades her father to let him stay for one night. Her good nature, love and sympathy change the peddler’s heart. The next morning, he leaves before the ironmaster and his daughter return from church. But now he is a changed man. He leaves behind the money stolen from the old man. He also leaves a rattrap as a Christmas present for Edla. He has also written a letter to her in which he praises her kindness and sympathy. Thus the love and kindness shown to him finally change his heart and make him change his ways.
(फेरी वाला चूहेदानियाँ बेचता था। लेकिन वह इतना धन नहीं कमा सकता था कि उसका गुजारा चल सके। इसलिए प्रायः वह छोटी-मोटी चोरियाँ करता रहता था। एक रात एक बूढ़े आदमी ने उसे भोजन और रात बिताने के लिए आश्रय प्रदान किया। उसने उसके प्रति प्यार और सहानुभूति दिखाई। लेकिन फेरी वाला दगाबाज आदमी निकला। जाने से पहले, वह बूढ़े आदमी का धन चोरी कर लेता है। लेकिन कहानी के अन्त में वह पूरी तरह से परिवर्तित इन्सान लगता है। आयरन मास्टर की बेटी एडला के द्वारा प्रदर्शित प्यार और समझ के द्वारा उसके अन्दर मानवता के आधारभूत गुण जागृत हो जाते हैं। आयरन मास्टर उसको रात बिताने के लिए अपने घर आमंत्रित करता है। उसकी बेटी एडला उसके प्रति सहानुभूति और दया के भाव प्रकट करती है।
जब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उसे चले जाने के लिए कहता है। लेकिन एडला अपने पिता पर दबाव बनाती है कि वह उसे एक रात के लिए वहीं ठहरने दे। उसका अच्छा स्वभाव, प्यार और सहानुभूति फेरी वाले के हृदय को परिवर्तित कर देती है। अगली सुबह वह आयरन मास्टर और उसकी बेटी के चर्च से आने से पहले ही वह चला जाता है। लेकिन अब वह एक बदला हुआ इन्सान है। वह बूढ़े आदमी के यहाँ से चोरी किए हुए धन को वहीं छोड़ जाता है। वह एडला के लिए क्रिसमस के उपहारस्वरूप एक चूहेदानी छोड़ जाता है। उसने उसे एक पत्र भी लिखा है जिसमें उसने उसकी दयालुता और सहानुभूति की प्रशंसा की। इस तरह से उसके प्रति दिखाए गए प्यार और दयालुता ने अंततः उसके हृदय को बदल दिया और उसे अपने तौर-तरीकों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया।)
Question 5.
How does the metaphor of the rattrap serve to highlight the human predicament? (चूहेदानी का रूपक किस प्रकार से मानवीय दुविधा को उजागर करता है ?)
Answer:
The title of the story ‘The rattrap’is highly metaphorical. The metaphor of the rattrap runs throughout the story. The writer uses this metaphor effectively. This metaphor highlights the human predicament. The story is based on a peddler who goes around selling rattraps. His life is poor and miserable. He does not earn enough money to keep his body and soul together. So he is compelled to beg or to commit petty thefts. One day, an idea comes to his mind that the whole world is a rattrap. In a rattrap the rat is caught while it tries to eat the bait. In the same way, the world sets baits for man to trap him. The riches, the joys, shelter, food, clothing, love, etc. are just baits. When a man attempts to get hold of these, he is caught in the rattrap of the world. Then everything comes to an end.
One night, an old man gives him food and shelter. The peddler sees his money in a pouch. That money lures him and the next morning, he steals the money. That was like a bait to him. Now he feels trapped. He dare not walk along the road for fear of being caught. He goes to a forest and loses his way. The forest appears like a rattrap to him. Then he goes to Ramsjö Ironworks and requests for shelter. The ironmaster invites him to his house. But the peddler does not want to fall into any fresh trouble. He thinks that going to his house is like falling into a den. So he emphatically refused to go with him. But when the ironmaster’s daughter insists, he goes with them. The next morning, he goes away and escapes being caught by police. Thus the metaphor of the rattrap highlights the predicament of the peddler.
(कहानी का शीर्षक ‘The Rattrap’ अति रूपकपूर्ण है। चूहेदानी का रूपक पूरी कहानी में बना रहता है। लेखक इस रूपक का बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है। यह रूपक मानवीय दुविधा का वर्णन करता है। यह कहानी एक फेरी वाले पर आधारित है जो कि इधर-उधर घूमकर अपनी चूहेदानियाँ बेचता है। वह गरीबी और कष्टों से पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। वह अपने आप को सही ढंग से जीवित रख पाने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं कमा सकता है। इसलिए वह भीख माँगने या फिर छोटी-मोटी चोरियाँ करने के लिए बाध्य हो जाता है। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आता है कि यह पूरा संसार एक चूहेदानी है। चूहेदानी में एक चूहा फंस जाता है जब वह रोटी के टुकड़े को खाने का प्रयास करता है। इसी तरह से, यह संसार भी इन्सान को फंसाने के लिए प्रलोभन पैदा करता है। अमीरी, खुशियाँ, घर, भोजन, वस्त्र, प्यार इत्यादि ऐसे ही कुछ प्रलोभन हैं। जब एक आदमी इनको हासिल करने का प्रयास करता है तो वह इस संसार की चूहेदानी में फंस जाता है। तब सब कुछ समाप्त हो जाता है।
एक रात, एक बूढ़ा आदमी उसको भोजन और आश्रय प्रदान करता है। फेरी वाला एक थैली में रखे उसके धन को देखता है। वह धन उसको ललचाता है और अगली सुबह वह उस धन को चोरी कर लेता है। यह उसके लिए एक प्रलोभन के समान था। अब वह फंसा हुआ महसूस करता है। पकड़े जाने के भय के कारण वह सड़क मार्ग से जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वह जंगल मार्ग से जाता है और रास्ता भटक जाता है। जंगल उसको एक चूहेदानी के समान प्रतीत होता है। तब वह रेमस्जो आयरन वर्क्स में जाता है और आश्रय के लिए निवेदन करता है। आयरन मास्टर उसे अपने घर आमंत्रित करता है। लेकिन फेरी वाला किसी नए संकट में नहीं फंसना चाहता है। वह सोचता है कि उसके घर जाना किसी गुफा में घुस जाने की तरह है। इसलिए वह जोर देकर उसके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन जब आयरन मास्टर की बेटी जाने के लिए जिद्द करती है तो वह चला जाता है। अगली सुबह, वह पुलिस के द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार से चूहेदानी का रूपक फेरी वाले की दुविधा को प्रकाशित करता है।)
Question 6.
The peddler comes out as a person with a great subtle sense of humour. How does this serve in lightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us?
(फेरी वाला हास्य की सूक्ष्म भावना वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। यह बात कहानी की गम्भीरता को किस प्रकार उजागर करती है और फेरी वाले को हमारे प्रति प्रिय बनाती है ?)
Answer:
This is a serious story and highlights the human predicament. Yet the peddler has a subtle sense of humour. He has a natural tendency to philosophize. It makes life less burdensome. His sense of humour makes him accept that he is like a rat like other people. He compares the world to a rattrap which sets baits for the people. The riches, the joys, the food, shelter, clothing and love are the things like baits. When a person tries to get them, he is caught in the rattrap.
The peddler’s meeting with the ironmaster is full of humour. The ironmaster mistakes him for his old friend. He addresses him as Captain von Stahle. This is humorous that a poor and uneducated peddler is mistaken as a captain. The peddler shows his senses of humour when he tells the ironmaster that he too “will get caught in the trap”. The ironmaster too accepts that it was “not so badly said.” His letter written to Edla also shows his sense of humour. He writes that he would have been caught in the rattrap if he had not been raised to captain. The peddler’s sense of humour serves to lighten the seriousness of the theme of the story. It also endears the peddler to the readers and evokes our sympathy for him.
(यह एक गंभीर कहानी है और मानव की दुविधा पर प्रकश डालती है। यद्यपि फेरी वाला हास्य की एक सूक्ष्म धारणा वाला व्यक्ति है। लेकिन उसमें वैचारिक सिद्धान्त का एक स्वभाविक गुण है। वह जीवन को कम बोझिल बनाता है। उसकी हास्य की भावना उससे स्वीकार करवा लेती है कि वह भी अन्य लोगों की तरह एक चूहा है। वह इस संसार की तुलना चूहेदानी से करता है जो लोगों को फंसाने के लिए प्रलोभन तय करता है। अमीरी, खुशियाँ, भोजन, घर, वस्त्र और प्यार प्रलोभन जैसी चीजें हैं। जब कोई व्यक्ति इनको हासिल करने का प्रयास करता है तो वह इसमें फंस जाता है। फेरी वाले की आयरन मास्टर से मुलाकात हास्य से भरपूर है। आयरन मास्टर उसे गलती से अपना पुराना मित्र समझ बैठता है। वह उसे कैप्टन वॉन स्टैहल कह कर सम्बोधित करता है। यह बात हास्य पैदा करने वाली है कि एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को गलती से कैप्टन समझ लिया जाता है। फेरी वाला अपनी हास्य की भावना का प्रदर्शन करता है जब वह आयरन मास्टर को बताता है कि वह भी “चूहेदानी में फंस जाएगा” । आयरन मास्टर भी इस बात को स्वीकार करता है कि यह बात “इतनी बुरी तरह से नहीं कही गई”। फेरी वाले के एडला को लिखे पत्र में उसकी हास्य की भावना का प्रदर्शन होता है। वह लिखता है कि वह भी चूहेदानी में फंस जाता यदि वह कैप्टन के पद से ऊपर न उठ जाता। फेरी वाले की हास्य की भावना इस कहानी के विषय की गम्भीरता को हल्का करने का काम करती है। यह भावना फेरी वाले को पाठकों में लोकप्रिय बनाती और उसके प्रति हमारी सहानुभूति को जागृत करती है।)

Think As You Read
Question 1.
From where did the peddler get the idea of the world being a rattrap? (फेरी वाले के दिमाग में यह विचार कैसे आया कि संसार एक चूहेदानी है?) Or Why did the peddler think that the world was a rattrap ? [H.B.S.E. March, 2019 (Set-C)] (फेरी वाले ने ऐसा क्यों सोचा कि संसार एक चूहेदानी है?)
Answer:
The peddler made his living by selling rattraps. But he did not earn much and often had to remain hungry. One day he was struck by an idea. He thought that the world was also like a rattrap. A rat is caught in the rattrap when it is lured by the bait. In the same way the world existed only to set baits for people. The world offers its riches, joys, shelter, food and clothing to man just to trap him.
(फेरी वाला चूहेदानियाँ बेचकर अपनी आजीविका कमाता था। लेकिन वह अधिक नहीं कमा पाता था और उसे प्रायः भूखा रहना पड़ता था। एक दिन उसको एक विचार सूझा। उसने सोचा कि यह संसार भी एक चूहेदानी के समान है। एक चूहा चूहेदानी के अंदर फंस जाता है जब वह खाने की चीज के लालच में आ जाता है। इसी तरह से यह संसार भी लोगों के लिए प्रलोभन पैदा करता रहता है। यह संसार मनुष्य को फंसाने के लिए अमीरी, खुशियाँ, घर, भोजन और वस्त्रों इत्यादि के प्रलोभन पैदा करता रहता है।)
Question 2.
Why was he amused by this idea? (वह इस विचार से प्रसन्न क्यों हुआ ?)
Answer:
One day an idea came to the mind of the rattrap seller that the whole world was also a rattrap. He was amused by this idea. He thought that the world’s joys, shelter, food, heat, clothing and riches were only baits to trap the people in. He was amused by the idea because he could philosophise his sad and boring life. The idea gave him satisfaction that he was not the only one in this world who was caught in the rattrap of poverty and misery.
(एक दिन चूहेदानियाँ बेचने वाले के दिमाग में एक विचार आया कि यह सारा संसार एक चूहेदानी के समान है। इस विचार से वह प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि संसार की खुशियाँ, घर, भोजन, ऊर्जा, वस्त्र और अमीर लोगों को फंसाने के लिए केवल एक प्रलोभन का काम करती है। वह इस विचार से प्रसन्न था क्योंकि वह अपने उदास और निराश जीवन को इस दर्शन (विचार) के साथ जोड़ सकता था। इस विचार ने उसको सन्तुष्टि प्रदान की कि इस संसार में वही केवल अकेला व्यक्ति नहीं है जो गरीबी और कष्टों की चूहेदानी में फंसा हुआ है।)
Question 3.
Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? (क्या फेरी वाले को उस आतिथ्य की आशा थी जो उसे बूढ़े किसान से प्राप्त हुआ ?)
Answer:
No, he did not expect the kind of hospitality that he received from the crofter. He only expected sour faces greeting him when he knocked at the door to ask for shelter for the night. But the old crofter was happy to get someone to talk to in his loneliness. He fed the peddler and played a game of cards with him until bed time.
(नहीं, उसने इस प्रकार के अतिथि सत्कार की कल्पना नहीं की थी। जैसा कि उसको किसान की ओर से मिला था। उसने केवल रूखे चेहरों के द्वारा अपना स्वागत किए जाने की कल्पना की थी जब रात के समय आश्रय के लिए उसने एक घर के दरवाजे को खटखटाया था। लेकिन बूढ़ा किसान अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए पाकर प्रसन्न था। उसने फेरी वाले को भोजन खिलाया और रात को सोने के समय तक उसके साथ ताश खेली।)
Question 4.
Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? (किसान फेरी वाले के साथ इतना बातूनी एवं दोस्ताना क्यों था ?) [H.B.S.E. March, 2018 (Set-C)]
Answer:
The old crofter welcomed the peddler. He was a lonely old man. He was without wife or children. He wanted someone to talk to in his loneliness. So he was so talkative and friendly with the peddler.
(बूढ़े किसान ने फेरी वाले का स्वागत किया। वह एक अकेला वृद्ध आदमी था। वह पत्नी और बच्चों को बिना रहता था। वह चाहता था कि उसके अकेलेपन में कोई उससे बात करने वाला हो। इसलिए वह फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी एवं दोस्ताना था।)

Question 5.
Why did he show the thirty kronor to the peddler? (उसने फेरी वाले को तीस क्रॉनर क्यों दिखाए ?)
Answer:
The old crofter told the peddler that he earned his living by selling his cow’s milk. Then he went to the window and took down a leather pouch hanging on a nail. He took out three ten-kronor notes to him. He wanted to show the peddler that although he was old and lonely, he was not without any means of income. He had a small income with which he could make both ends meet.
(उसने फेरी वाले को बताया कि वह अपनी गाय का दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता है। तब वह खिड़की के पास गया और एक कील पर टंगी हुई चमड़े की थैली उतार कर के लाया। उसने दस क्रॉनर के तीन नोट उसे निकाल कर दिखाए। वह फेरी वाले को दिखाना चाहता था कि यद्यपि वह बूढ़ा और अकेला है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। उसकी थोड़ी-सी आमदनी थी जिसकी वजह से उसका हर रोज का गुजारा चल जाता था।)
Question 6.
Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter ? (क्या फेरी वाले ने किसान द्वारा दर्शाए गए भरोसे का सम्मान किया ?)
Answer:
The peddler was a stranger to the old crofter. But he did not suspect him. He showed him the thirty kronors which he had in a leather pouch. He trusted the peddler. But the peddler did not respect the confidence reposed in him. After the crofter had left the cottage, the peddler went back. He broke a window pane and caught hold of the leather pouch. He took out the money. In this way, he robbed the man who had given him food and shelter.
(फेरी वाला बूढ़े किसान के लिए एक अजनबी था। लेकिन उसने उस पर संदेह नहीं किया। उसने उसको वो तीस क्रॉनर दिखाए जो उसने चमड़े की थैली में रखे हुए थे। वह फेरी-वाले पर यकीन करता था। लेकिन फेरी वाले ने अपने ऊपर दिखाए गए विश्वास का सम्मान नहीं किया। जब किसान घर से बाहर चला गया, तो फेरी वाला वहाँ वापस गया। उसने खिड़की का एक काँच तोड़ा और चमड़े की थैली को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने पैसे निकाल लिए इस तरह से, उसने उस आदमी को ठग लिया जिसने उसे भोजन और आश्रय दिया था।)
Question 7.
What made the peddler think that he had indeed fallen into a rattrap? (फेरी वाले ने ऐसा क्यों सोचा कि वह सचमुच चूहेदानी में फँस गया है ?)
Answer:
The peddler stole the old crofter’s money. In order to avoid being caught, he did not walkalong the main road. He entered a forest. But he lost the way. In the meantime, the night fell and it was very cold. He sat down on the ground. Now he thought that the world was indeed a rattrap. The money was only a bait to catch him.
(फेरी वाले ने किसान का धन चोरी कर लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए, वह मुख्य मार्ग से नहीं गया। उसने एक जंगल में प्रवेश किया। लेकिन वह रास्ता भटक गया। इतनी देर में रात हो गई और ठंड भी बहुत अधिक थी। वह जमीन पर नीचे बैठ गया। अब उसने सोचा कि वह संसार सचमुच में ही एक चूहेदानी है। यह धन भी उसको शिकंजे में लेने के लिए एक प्रलोभन है।)
Question 8.
Why did the ironmaster speak kindly to the peddler and invite him home? (आयरन मास्टर फेरी वाले से दयालुता से क्यों बोला और उसे अपने घर क्यों बुलाया ?)
Answer:
When the ironmaster saw the peddler, he thought that he was one of his old friends. He mistook him for an old friend. The ironmaster was an old man. There was no one at his home except his eldest daughter. It was too bad that he didn’t have company for the Christmas night. So he spoke kindly to him and invited him to his house for the night.
(जब आयरन मास्टर ने फेरी वाले को देखा तो उसने सोचा कि वह उसका कोई पुराना मित्र है। उसने गलती से उसे अपना एक पुराना मित्र समझ लिया। आयरन मास्टर एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सबसे बड़ी बेटी के सिवाय उसके घर पर और कोई नहीं था। यह उसके लिए बहुत बुरा था कि क्रिसमस की रात में साथ रहने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। इसलिए उसने उसके साथ दयालुतापूर्वक बात की और रात बिताने के लिए उसे अपने घर पर आमंत्रित किया।)

Question 9.
Why did the peddler decline the invitation? [H.B.S.E. 2017 (Set-B), 2019 (Set-D)] (फेरी वाले ने निमन्त्रण क्यों ठुकरा दिया ?) [H.B.S.E. 2020 (Set-C)]
Answer:
The ironmaster invited the peddler to spend the night with him at his home. But the peddler felt alarmed. The ironmaster was a stranger to him. He thought that going with him to his home was like throwing himself into a lion’s den. He didn’t want to be caught in. So he declined the ironmaster’s invitation.
(आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर पर उसके साथ रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन फेरी वाला डरा हुआ था। आयरन मास्टर उसके लिए एक अजनबी था। उसने सोचा कि उसके साथ उसके घर जाना स्वयं को एक शेर की गुफा में घुसा देने के समान है। वह पकड़ा नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने आयरन मास्टर के निमंत्रण को ठुकरा दिया।)
Question 10.
What made the peddler accept Edla Willmansson’s invitation ? (फेरी वाले ने एडला विलमैनसन के निमन्त्रण को स्वीकार क्यों कर लिया ?)
Answer:
The ironmaster mistook the peddler for one of his old friends. He invited the peddler to his home. But the peddler declined the invitation. Then the ironmaster’s young daughter Edla Willmansson came. She did not hate him for his shabby clothes. She looked at him compassionately. He requested him to stay with them on the Christmas Eve. Her manner was so friendly that the peddler accepted the invitation.
(आयरन मास्टर ने फेरी वाले को गलती से अपना एक मित्र मान लिया। उसने फेरी वाले को अपने घर आमंत्रित किया। लेकिन फेरी वाले ने उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया। तब आयरन मास्टर की छोटी लड़की एडला विलमैनसन वहाँ आई। वह उसके गंदे कपड़ों की वजह से उससे घृणा नहीं कर रही थी। उसने दया भाव के साथ उसकी ओर देखा। उसने उससे प्रार्थना की कि वह क्रिसमस की शाम उनके साथ बिताए। उसका भाव इतना मित्रतापूर्ण था कि फेरी वाले ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।)
Question 11.
What doubts did Edla have about the peddler? [H.B.S.E. 2017 (Set-C), 2018 (Set-B)] (एडला को फेरी वाले के बारे में क्या सन्देह था ?)
Answer:
When Edla saw the peddler and his shabby conditions, she had her own doubts about him. She thought that perhaps he had stolen something. It was possible that he had escaped from prison. He did not look like an educated man. That is why, she had doubts about the peddler.
(जब एडला ने फेरी वाले और उसकी गंदी हालत को देखा, तो उसके मन में उसके प्रति संदेह पैदा हो गए। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ चोरी किया हुआ है। इस बात की भी संभावना थी कि शायद वह जेल से बचकर निकला हो। वह एक पढ़े-लिखे इन्सान जैसा नहीं लगता था। इसी वजह से, उसके मन में फेरी वाले के प्रति संदेह थे।)
Question 12.
When did the ironmaster realise his mistake? [H.B.S.E. 2017 (Set-D), 2018 (Set-A)] (आयरन मास्टर को अपनी भूल का एहसास कब हुआ ?)
Answer:
The ironmaster took the peddler home. The next morning, his valet bathed and shaved him. He stood in front of him in broad daylight. Now everything became clear. The ironmaster realised that he had made a mistake about him. He was not his old regimental comrade.
(आयरन मास्टर फेरी वाले को घर ले गया। अगली सुबह उसके नौकर ने उसे स्नान करवाया और उसकी दाढ़ी बनाई। वह सूर्य के प्रकाश में उसके सामने खड़ा था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। आयरन मास्टर को एहसास हो गया था कि उसने उसके बारे में गलती कर दी है। वह उसकी रेजिमेंट का उसका पुराना साथी नहीं था।)’
Question 13.
What did the peddler say in his defence when it was clear that he was not the person the ironmaster had thought he was? (जब यह मालूम हो गया कि फेरी वाला वह नहीं है जो उसके बारे में सोचा गया था तो उसने अपने बचाव में क्या कहा ?)
Answer:
In the broad daylight, it became clear to the ironmaster, the peddler was not his old comrade. He told him that he would hand him over to the sheriff. At this, the peddler said in his defence that he never tried to cheat him. He never pretended to be his friend. He insisted that he was only a poor rattrap seller. But they insisted on bringing him home and giving him shelter.
(दिन के प्रकाश में आयरन मास्टर को यह बात साफ हो गई कि फेरी वाला उसका पुराना मित्र नहीं था। उसने उसे बताया कि वह उसे शेरिफ के हवाले कर देगा। इस बात पर फेरी वाले ने अपने बचाव में कहा कि उसने कभी भी उसे धोखा देने का प्रयास नहीं किया। उसने कभी भी उसका मित्र होने का ढोंग नहीं किया। उसने जोर देकर कहा कि वह तो मात्र एक गरीब चूहेदानियाँ बेचने वाला है। लेकिन वे उसे घर लाने और आश्रय प्रदान करने की जिद्द करते रहे।)
Question 14.
Why did Edla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? (जब एडला को फेरी वाले की वास्तविकता का पता चल गया तो उसके बाद भी उसने उसका स्वागत क्यों किया ?)
Answer:
The peddler’s identity was revealed. The ironmaster asked him to go away. But his daughter, Edla still entertained him. She felt sorry for him. She told her father that the peddler was not welcome anywhere. She wanted that he should enjoy a day’s peace with them. Moreover, they themselves had invited him and promised Christmas cheer. Now it was wrong to chase him away.
(फेरी वाले की वास्तविकता का पता चल चुका था। आयरन मास्टर ने उसे चले जाने के लिए कहा। लेकिन उसकी बेटी एडला अभी भी उससे अच्छी तरह से बातचीत कर रही थी। उसे उसके प्रति खेद हो रहा था। उसने अपने पिता को बताया कि फेरी वाले का कहीं भी स्वागत नहीं है। वह चाहती थी कि वह एक दिन के लिए उनके साथ चैन से रहे। और उन्होंने स्वयं ही उसको आमंत्रित किया था और उसके साथ आनंदपूर्वक क्रिसमस का वायदा किया था। अब उसे वहाँ से भगा देना गलत बात थी।)

Question 15.
Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? [H.B.S.E. 2019 (Set-B), 2020 (Set-D)] (फेरी वाले द्वारा छोड़ा गया उपहार देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई ?)
Answer:
Although the peddler’s identity had been revealed, Edla had insisted that he should stay them for the night. The next morning at the church, she came to know that the peddler had robbed an old man. Her father was sure that in their absence, he might have stolen their silver spoons. But when they came back Edla found that the peddler had not taken anything away. On the other hand he had left a rattrap as a gift for her. He had also left the thirty kronors that he had stolen from the old crofter. In his letter, the peddler had praised Edla and her hospitality. So, Edla was happy to see the gift left by him.
(यद्यपि फेरी वाले की वास्तविकता का पता चल गया था, फिर भी एडला इस बात पर बल दे रही थी कि वह रात को तो उनके साथ ही रहे। अगली सुबह चर्च में, उसको इस बात का पता चला कि उसने एक बूढ़े आदमी को ठगा है। उसके पिता को इस बात का यकीन था कि उनकी गैर हाजरी में वह उनके चाँदी के चम्मचों को चुरा सकता था। लेकिन जब वे लौटकर आए तो एडला ने देखा कि फेरी वाला कुछ भी चुराकर नहीं ले गया था। बल्कि वह उसके लिए उपहारस्वरूप एक चूहेदानी छोड़कर गया था। वह उन तीस क्रॉनर को भी वहीं छोड़कर चला गया था जो उसने बूढ़े किसान के घर से चोरी किए थे। अपने पत्र में फेरी वाले ने एडला की और उसके अतिथि सत्कार की भावना की प्रशंसा की थी। इसलिए एडला उसके द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर प्रसन्न थी।)
Question 16.
Why did the peddler sign himself as Captain Von Stahle? [H.B.S.E. 2019 (Set-C)] (फेरी वाले ने अपने हस्ताक्षर कप्तान वॉन स्टाहल के रूप में क्यों किए ?)
Answer:
The peddler was a poor vagabond. But the ironmaster mistook him to be his old friend Captain von Stahle. He and his daughter treated him with kindness. They invited him to his house and fed and clothed him. When the ironmaster realised his mistake he asked him to go away. But his daughter, Edla insisted on his staying there. The kindliness and sympathy shown to him by Edla moved his heart. So he signed himself as Captain von Stahle in appreciation of the love that he received there.
(फेरी वाला एक गरीब घुमक्कड़ था। लेकिन आयरन मास्टर ने गलती से उसे अपना एक पुराना मित्र कैप्टन वॉन स्टाहल समझ लिया। उसने और उसकी बेटी ने उसके साथ दयालुतापूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने उसे अपने घर आमंत्रित किया। उसे भोजन खिलाया और वस्त्र दिए। जब आयरन मास्टर को अपनी गलती का पता चला तो उसने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। लेकिन उसकी बेटी एडला इस बात की जिद्द करती रही कि वह वहीं पर रहे। एडला के द्वारा दिखाई गई दया और सहानुभूति ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया। इसलिए उसने वहाँ मिले प्यार की प्रशंसा में वॉन स्टाहल के रूप में अपने हस्ताक्षर किए।)
Talking About The Text
Question 1.
The reader’s sympathy is with the peddler right from the beginning of the story. Why is this so? Is the sympathy justified?
(कहानी के आरम्भ से ही पाठकों की सहानुभूति फेरी वाले के साथ है। ऐसा क्यों है? क्या यह सहानुभूति उचित है?)
Answer:
The rattrap seller is a very poor man. He goes from village to village selling rattraps. But he does not earn enough to keep his body and soul together. So he resorts to begging and petty thefts. We know that stealing is a crime. Yet the readers do not hate him. They have sympathy for him. We know that he is not a habitual thief. If he had been a habitual thief, he would have committed big thefts and there would have been no need for him to wander here and there selling rattraps. He commit thefts only when he has nothing to eat. Although he is a poor, he is a thinker. He can philosophise about his condition. He steals the money of the old crofter. But the feeling of guilt remains with him. When Edla shows love and sympathy to him, he repents at his deed. He leaves the money and requests Edla her to return it to the old man. Thus our sympathy for him is justified. We know that he is not bad at heart. He is only a victim of circumstances.
(चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब आदमी है। वह गाँव दर गाँव चूहेदानियाँ बेचने जाता है। लेकिन वह अपने आप को ठीक ढंग से जिन्दा रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाता है। इसलिए वह भीख माँगने और छोटी-मोटी चोरियाँ करने का काम करने लग जाता है। हम जानते हैं कि चोरी करना एक अपराध है। फिर भी पाठक चोरीवाले से घृणा नहीं करते हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। हम जानते हैं कि वह एक पेशेवर चोर नहीं है। यदि वह एक पेशेवर चोर होता, तो वह बड़ी चोरियाँ करता और फिर उसको इधर-उधर घूमकर चूहेदानियाँ बेचने की जरूरत न होती। वह तभी चोरियाँ करता है जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यद्यपि वह एक गरीब है, लेकिन वह एक विचारक भी है। वह अपनी स्थिति पर विचार कर सकता है। वह बूढ़े किसान का धन चुराता है। लेकिन इस अपराध का बोध उसमें बना रहता है। जब एडला उसके प्रति प्यार और सहानुभूति प्रदर्शित करती है, तो उसे अपने काम पर पछतावा होता है। वह धन को छोड़ जाता है और एडला से प्रार्थना करता है कि वह उस धन को बूढ़े किसान को लौटा दे। अतः उसके प्रति हमारी सहानुभूति न्याय संगत है। हम जानते हैं कि वह दिल से बुरा नहीं है। वह तो केवल परिस्थितियों का शिकार है।)
Question 2.
The story also focuses on human loneliness and the need to bond with others. (कहानी मानवीय अकेलेपन एवं दूसरों के मिलने की उसकी जरूरत पर भी केन्द्रित है।)
Answer:
This story focuses on human loneliness and his need to bond with the others. Man is a social animal. He cannot live in isolation. We feel sympathy for the rattrap seller as he is a lonely and miserable man. He leads a sad and monotonous life. He goes from place to place, selling rattraps. One evening he sees a cottage by the side of a road. He knocks at the door in the hope of getting food and shelter. An old crofter lives there. He is also lonely. He is without wife or child. So he welcomes the peddler.
He offers him food and shelter. He is happy to see the stranger because he can talk to him. He plays a card of game with him until the bedtime. The ironmaster is also lonely, although his daughter lives with him. So he also welcomes the peddler. He tells him that he and his daughter were feeling bad because they did not have company for the Christmas. His daughter insists on his coming to stay with them for the night. Thus the story focuses on human loneliness. It highlights man’s need to bond with others.
(यह कहानी मानव के एकाकीपन और उसके दूसरों के साथ रिश्तों की जरूरत पर केंद्रित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेलेपन में नहीं रह सकता है। हमें चूहेदानियाँ बेचने वाले के प्रति सहानुभूति होती है क्योंकि वह एक अकेला और दुखी आदमी है। वह एक उदासी और नीरसता भरा जीवन व्यतीत करता है। वह चूहेदानियाँ बेचने के लिए जगह-जगह जाता है। एक शाम उसे एक सड़क किनारे एक घर दिखाई देता है। वह भोजन और आश्रय पाने की उम्मीद के साथ उस घर का दरवाजा खटखटाता है। वहाँ एक बूढ़ा किसान रहता है। वह भी अकेला है। वह पत्नी या बच्चे के बिना रहता है। इसलिए वह फेरी वाले का स्वागत करता है। वह उसे भोजन और आश्रय प्रदान करता है।
वह अजनबी को देखकर प्रसन्न है क्योंकि वह उससे बात कर सकता है। वह सोने के समय तक उसके साथ ताश खेलता है। आयरन मास्टर भी अकेला है, यद्यपि उसकी बेटी उसके साथ रहती है। इसलिए वह भी फेरी वाले का स्वागत करता है। वह उसे बताता है कि उसे और उसकी बेटी को बुरा लग रहा है क्योंकि क्रिसमस पर उनके साथ कोई भी साथ देने वाला नहीं है। उसकी बेटी उसके साथ जिद्द करती है कि वह आकर उनके साथ रात बिताए। इस तरह से यह कहानी मानव के एकाकीपन पर केंद्रित है। यह मनुष्य की दूसरों के साथ रिश्तों के महत्व पर प्रकाश डालती है।)
Question 3.
Have you known/heard of an episode where a good deed or an act of kindness has changed a person’s view of the world? (क्या आपने ऐसी किसी घटना को देखा/सुना है जहाँ किसी व्यक्ति के दया के काम ने अन्य व्यक्ति के संसार के बारे के दृष्टिकोण को बदल दिया हो।)
Answer:
For self attempt with the help of the teacher and classfellows.

Question 4.
The story is both entertaining and philosophical. (कहानी मनोरंजनपूर्ण एवं दार्शनिकतापूर्ण दोनों ही है।)
Answer:
The ‘Rattrap’ is an interesting story. It is entertaining as it presents the story of a poor peddler who goes around selling rattraps. He also commits a theft. There is an element of suspense as the reader does not know whether he will be caught or not. At the same time, the story is philosophical also. The peddler is in the habit of philosophising his misery. One day an idea comes to his mind that the world is also a rattrap. It sets baits for people and then traps them. The world offers riches and joys, food and shelter, heat and clothing to man.
As soon as man is tempted to take these things, the world traps him. And there is no escape from this trap. The rattrap seller is tempted to steal the money of an old man who gives him shelter. Then the peddler escapes to a forest. There he loses his way and thinks that the forest is a rattrap. Later when the ironmaster invites him to his house, he feels that he is going into another rattrap. Another philosophical idea in the story is that love and understanding can awaken man’s essential goodness. The sympathy shown by Edla to the peddler changes his heart.
(‘The Rattrap’ एक रोचक कहानी है। यह मनोरंजक है क्योंकि यह एक गरीब फेरी वाले की कहानी प्रस्तुत करती है जो चूहेदानियाँ बेचने के लिए इधर-उधर जाता है। वह एक चोरी भी करता है। इस कहानी में एक रहस्य भी है क्योंकि पाठक यह नहीं जानता है कि वह पकड़ा जाएगा या नहीं। साथ-ही-साथ यह कहानी दार्शनिकतापूर्ण भी है। फेरी वाला अपने दुखों के बारे में विचार करता है। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आता है कि यह संसार एक चूहेदानी के समान है। यह लोगों के लिए प्रलोभन देता है और उनको फंसा लेता है। यह संसार (आदमी को) अमीरी और खुशियाँ, भोजन और आश्रय तथा ऊर्जा और वस्त्र प्रदान करता है। जैसे ही इन्सान इन चीजों को हासिल करने के लिए लालच में आता है तो संसार उसे फंसा लेता है और इस चंगुल से छूटने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
चूहेदानियाँ बेचने वाला एक बूढ़े किसान का धन चोरी कर लेता है जो कि उसे आश्रय देता है। तब फेरी वाला एक जंगल के रास्ते से बचकर निकलता है। वहाँ वह रास्ता भटक जाता है और सोचता है कि यह संसार एक चूहेदानी के समान है। बाद में जब आयरन मास्टर उसे अपने घर आमंत्रित करता है, तो वह सोचता है कि वह एक अन्य चूहेदानी में फंसने जा रहा है। इस कहानी का दूसरा दार्शनिकता वाला विचार यह है कि प्यार और समझ इन्सान की अच्छाइयों को जागृत कर देती है। एडला के द्वारा फेरी वाले के प्रति दर्शाई गई सहानुभूति उसके हृदय को परिवर्तित कर देती है।)
Working With Words
Question 1.
The man selling the rattraps is referred to by many terms as ‘peddler,’ ‘stranger’, etc. Pick out all such references to him. What does each of these labels indicate of the context or the attitude of the people around him.
(चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी का जिक्र कई नामों से किया गया है, जैसे कि ‘फेरी वाला’, ‘अजनबी’, आदि। उसके बारे में सारे ऐसे नामों को ढूँढो। इनमें से प्रत्येक नाम, सन्दर्भ एवं उसके आस-पास के लोगों के बारे में क्या बताता है ?)
Answer:
The man selling the rattraps is referred to by many names. First of all, he is referred to as a ‘vagabond’. He has no permanent residence and wanders from place to place. He goes around selling rattraps. He seeks shelters wherever the night falls. Then an old crofter gives him food and shelter. Now he is referred to as a ‘stranger’. It is because the old crofter does not know him. He is a stranger to him. He is called the man with the rattraps’ because he sells rattraps. He is also referred to as the rattrap peddler’, because he is a travelling hawker who goes from village to village selling rattraps. He is called a “tramp’ because he is a wanderer.
When the ironmaster first saw him, he thought that he was a ‘tall ragamuffin’ because he was a tall man dressed in ragged clothes. Then the ironmaster mistakes him for his old friend and calls him his ‘old regimental comrade.’ When he refers to the whole world being a rattrap, the ironmaster laughs and calls him a “good fellow’. His daughter Edla refers to him as “the poor hungry wretch”. Thus he is given different labels accofding to the attitude of the people around him.
(चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी को कई नामों से सम्बोधित किया गया है। सबसे पहले तो उसको एक घुमक्कड़ के रूप में सम्बोधित किया गया है। उसका कोई स्थाई आवास नहीं है और वह जगह-जगह भटकता फिरता है। वह चारों ओर चूहेदानियाँ बेचता फिरता है। जहाँ कहीं रात पड़ जाती है वह वहीं आश्रय ले लेता है। तब एक बूढ़ा किसान उसको भोजन और आश्रय प्रदान करता है। फिर उसको एक अजनबी के रूप में सम्बोधित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बूढ़ा किसान उसे जानता नहीं है। वह उसके लिए एक अजनबी है। उसे चूहेदानियों वाला आदमी भी कहा गया है क्योंकि वह चूहेदानियाँ बेचता है। उसे फेरी वाला भी कहा गया क्योंकि वह इधर-उधर घूमकर फेरी लगाने वाला व्यक्ति है जो गाँव दर गाँव चूहेदानियाँ बेचने के लिए घूमता रहता है। उसे एक ‘अवारा’ भी कहा गया है क्योंकि वह घूमने-फिरने वाला व्यक्ति है।
जब आयरन मास्टर ने पहली बार उसे देखा, तो उसने सोचा कि वह एक लम्बा भिखारी है क्योंकि वह एक लम्बा आदमी था जिसने फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थे। तब आयरन मास्टर उसको गलती से अपना पुराना मित्र मान लेता है और उसे अपना सेना का पुराना मित्र बताता है। जब वह सारे संसार को एक चूहेदानी बताता है तो आयरन मास्टर उसको एक ‘अच्छा इन्सान’ कहता है। उसकी बेटी एडला उसको एक “गरीब भूखा आदमी” कहती है। इस तरह से उसको उसके आस-पास के लोगों के द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है।)
Question 2.
You came across the words, ‘plod’, ‘trudge’, ‘stagger’ in the story. These words indicate movement accompanied by weariness. Find five other such words with a similar meaning. (आपको कहानी में ‘प्लॉड’, ‘ट्रज’, ‘स्टैगर’ जैसे शब्द नजर आते हैं। ये शब्द थकानपूर्ण चाल को दर्शाते हैं। इन्हीं अर्थों वाले ऐसे अन्य शब्द ढूँढो।)
Answer:
slog, drag, lurch, sway, wobble.
Noticing Form
1. He made them himself at odd moments.
2. He raised himself.
3. He had let himself be fooled by a bait and had been caught.
4…. a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork. Notice the way in which these reflexive pronouns have been used (pronoun + self).
In 1 and 4 the reflexive pronouns “himself” and “yourself” are used to convey emphasis.
In 2 and 3 the reflexive pronoun is used in place of personal pronoun to signal that it refers to the same subject in the sentence.
Pick out other examples of the use of reflexive pronouns from the story and notice how they are used.
Answer:
(i) He let himself be tempted to touch the bait.
Here “himself” has been used in place of a personal pronoun to show that it refers to the same subject that is ‘He’ in the sentence.
(ii) He laughed to himself. It is used to show that it refers to the same subject in the sentence.
(iii) It would never occurred to me that ‘you would bother with me yourself’; It refers to the same subject in the sentence.
(iv) He could not bring himself to oppose her. It refers to the same subject in the sentence.
Thinking About Language
Question 1.
Notice the words in bold in the following sentence.
“The fire boy shovelled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter.” This is a phrase that is used in the specific context of an iron plant. Pick out other such phrases and words from the story that are peculiar to the terminology of ironworks.
Answer:
(a) A hard regular thumping.
(b) Those are the hammer strokes from an iron mill.
(c) ………………. with smelter, rolling mill, and forge.
(d) Master Smith and his helper sat in the dark forge near the furnace.
(e) Waiting for the pig iron
(f) ……… to be ready to put on the anvil.
(g) …. to stir the glowing mass
(h) The big bellows groaned.
(i) The burning cool cracked.
Question 2.
“Mjölis” is a card game of Sweden. Name a few indoor games played in your region. “Chopar” could be an example.
Answer:
ludo, carom, table tennis, chess, etc.

Question 3.
A “Crofter” is a person who rents or owns a small farm, especially in Scotland. Think of other uncommon terms for “a small farmer” including those in your language.
Answer:
granger, planter, tiller, cultivator, ranchman, grower, ‘Kisan, “khetihar’, etc.
HBSE 12th Class English The Rattrap Important Questions and Answers
Short Answer Type Questions
Answer the following questions in about 20-25 words :
Question 1.
Did the rattrap peddler earn enough money to keep his body and soul together? (क्या चूहेदानी बेचने वाला जीवित रहने के लिए पर्याप्त धन कमा लेता है ?)
Answer:
No, the rattrap peddler did not earn enough money to make both ends meet. He went from place to place selling the rattraps. Yet the business was not good. He was always in rags. His cheeks were sunken and he often remained hungry. Sometimes he had to resort to begging or stealing in order to remain alive.
(नहीं, फेरी वाला इतना धन नहीं कमा सकता था जिससे उसका गुजारा हो सके। वह चूहेदानियाँ बेचने के लिए जगह-जगह जाता था। फिर भी उसका धंधा अच्छा नहीं था। वह फटे-पुराने कपड़े पहनता था। उसकी गालें चिपकी हुई थीं और वह हमेशा भूखा रहता था। कई बार तो उसको जिंदा रहने के लिए भीख माँगनी पड़ती थी या चोरी करनी पड़ती थी।)
Question 2.
What philosophical idea came to the peddler’s mind one day? (एक दिन फेरी वाले के दिमाग में क्या दार्शनिक विचार आया ?)
Answer:
One day, while selling rattraps, an idea struck his mind. He thought that the whole world is also like a rattrap. In a rattrap, the rat is caught when he is attracted to the bait and tries to eat it. In the same way the world sets baits for people. These baits are riches, joys, shelter, food and clothing. When a person is tempted towards these bats, he is caught like a rat.
(एक दिन, चूहेदानियाँ बेचते समय उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि सारा संसार ही एक चूहेदानी के समान है। चूहेदानी में चूहा फंस जाता है जब वह भोजन के लालच में आ जाता है और उसे खाने का प्रयास करता है। इसी तरह से यह संसार भी लोगों के लिए प्रलोभन प्रस्तुत करता है। अमीरी, खुशियाँ, घर, भोजन और कपड़े ऐसे ही कुछ प्रलोभन हैं। जब कोई इन्सान इन प्रलोभनों के लालच में आ जाता है, तो वह चूहे की तरह फंस जाता है।)
Question 3.
Where did the peddler seek shelter one evening? (एक शाम को फेरी वाले ने आश्रय की तलाश कहाँ की ?)
Answer:
One dark evening, the peddler was walking along the road with great difficulty. He noticed a little grey cottage by the roadside. He knocked on the door, an old man welcomed him. He was a crofter without wife or child. He gave shelter and food to the peddler.
(एक अंधेरी शाम को, फेरी वाला बड़ी कठिनाई से सड़क किनारे चला जा रहा था। उसने सड़क किनारे एक छोटा-सा स्लेटी रंग का घर देखा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, तो एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया। वह एक किसान था जिसकी पत्नी अथवा बच्चा नहीं थे। उसने फेरी वाले को भोजन अथवा आश्रय प्रदान किया।)

Question 4.
Why was the old crofter happy to see the peddler? (बूढ़ा किसान फेरी वाले को देखकर खुश क्यों हो गया ?) Or Why was the croften so talkative and friendly with the peddler? [H.B.S.E. March, 2019 (Set-D)] (किसान फेरीवाले के साथ इतना बातूनी और मैत्रीपूर्ण क्यों था?)
Answer:
The old crofter welcomed the poor peddler. He was happy to get someone to talk to in his loneliness. He fed the peddler and played a game of cards with him until bedtime. The old man told him that he had been a crofter at Ramsjö Ironworks.
(बूढ़े किसान ने फेरी वाले का स्वागत किया। वह अपने अकेलेपन में किसी को अपने साथ बात करने के लिए पाकर प्रसन्न था। उसने फेरी वाले को भोजन कराया और रात को सोने के समय तक उसके साथ ताश खेली। बूढ़े आदमी ने उसको बताया कि वह रेमस्जो आयरन वर्क्स में काम किया करता था।)
Question 5.
What did the peddler sell and how did he make those things ? [H.B.S.E. 2020 (Set-B)] (फेरीवाले ने क्या किया और उसने उन चीजों को कैसे बनाया?)
Answer:
The peddler sold small rattraps of wire. He made them himself at odd moments,from the material he got by begging in the stores or at the big farms.
(फेरीवाले ने तार की छोटी चूहेदानियाँ बेचीं। उसने उन्हें स्वयं उस सामग्री से अजीब क्षणों में बनाया जिसे उसने दुकानों या बड़े खेतों में भीख मांगकर प्राप्त किया था।)
Question 6.
How did the old crofter and the peddler leave the cottage the next morning? (बूढ़ा किसान एवं फेरी वाला कुटीर से अगली प्रातः कैसे बाहर गए ?)
Answer:
The next morning, the old crofter and the peddler left the cottage simultaneously. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The peddler thanked the old man and bade him good bye. Then they went their own ways. (अगली सुबह, किसान और फेरी वाला एक साथ घर से बाहर निकले। किसान ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। फेरी वाले ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और उसे अलविदा कहा। तब वे अपने-अपने रास्तों पर चले गए।)
Question 7.
How did the peddler steal the old crofter’s money? (फेरी वाले ने बूढ़े किसान का पैसा किस प्रकार चुराया ?)
Answer:
The next morning both the men left the cottage at the same time. But half an hour later, the peddler came back to the house. He went to window, smashed a pane and got hold of the pouch. He took out the money and hung the pouch back in its place. Then he went his way.
(अगली सुबह दोनों आदमी एक साथ घर से बाहर गए। लेकिन आधे घंटे बाद, फेरी वाला वापस घर लौट आया। वह खिड़की के पास गया, उसने एक शीशा तोड़ा और थैली अपने हाथ में ले ली। उसने धन बाहर निकाला और थैली को उसी स्थान पर टांग दिया। तब वह चला गया।)
Question 8.
After stealing the money, why did the peddler feel that he was trapped? (पैसा चुराने के बाद फेरी वाले ने ऐसा क्यों महसूस किया कि वह फँस गया है ?)
Answer:
With the stolen money in his pocket, it was not safe for the peddler to walk on the public highway. So he turned off the road into a forest. Later in the day he got into a big and confusing forest. He walked and walked without coming to the end of the forest. Now he felt that the world was really a big rattrap. The money he had stolen was the bait and he had been trapped.
(अपनी जेब में चोरी किया हुआ धन रखकर, फेरी वाले के लिए मुख्य मार्ग से सफर करना सुरक्षित नहीं था। इसलिए वह सड़क मार्ग को छोड़कर जंगल के रास्ते चल दिया। बाद में वह एक बड़े और उलझन वाले जंगल में प्रवेश कर गया। वह चलता गया, चलता गया लेकिन जंगल का अंत ही नहीं हुआ। अब उसको एहसास हो गया था कि यह संसार एक बड़ी चूहेदानी है। जो धन उसने चोरी किया था वह एक प्रलोभन के समान था और वह इसके जाल में फंस चुका था।)
Question 9.
What did the peddler hear when he had lost the hope of his survival? (जब फेरी वाले को जीवन की आशा खो गई महसूस हुई तो उसने क्या सुना ?)
Answer:
Darkness was descending. It was late in December and the forest was getting cold. When he had lost hope of survival, he heard a sound. It was the sound of hammer strokes coming from a iron mill. He got up and moved with difficulty towards the sound.
(अंधेरा घना होता जा रहा था। दिसम्बर के अंतिम दिनों की बात थी और जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी। जब उसने अपने जीवन की आशा खो दी तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक लोहे के कारखाने से हथौड़े के टकराने की आवाज थी। वह उठ खड़ा हुआ और कठिनाई के साथ उस आवाज की ओर बढ़ा।)
Question 10.
Why did the rattrap peddler take his way through forest ? [H.B.S.E. 2020 (Set-A)] (चूहेदानी बेचने वाले ने जंगल के माध्यम से अपना रास्ता क्यों बनाया?)
Answer:
The paddler made his living by selling rattraps. But he did not earn much and often had to remain hungry. So, one day he stole an old crofter’s money. In order to being caught, he did not walk along the main road and took his way to the forest.
(पैडलर ने चूहेदानियाँ बेचकर अपना जीवनयापन किया। लेकिन वह ज्यादा नहीं कमाता था और अक्सर भूखा रहना पड़ता था। इसलिए, एक दिन उसने एक पुराने क्रॉफ्टर का पैसा चुरा लिया। पकड़े जाने के डर से, वह मुख्य सड़क पर नहीं चलता था और जंगल में अपना रास्ता बनाता था।)
Question 11.
Why did the ironmaster come to the Ramsjö Ironworks in the night? (आयरन मास्टर रात को रेमस्जो आयरन वर्कस में क्यों आया ?)
Answer:
The ironmaster was the owner of the Ramsjö Ironworks. It was his ambition to ship out good iron to market. He supervised the work day and night in order to make sure that the work was going on well. That night also he had come to the ironworks for his round of inspection.
(आयरन मास्टर रेमस्जो आयरन वर्क्स का मालिक था। उसका लक्ष्य था अच्छी किस्म के लोहे को विदेशी बाजारों में भेजना। वह रात-दिन देखता था कि काम जितना सम्भव हो सके उतना अच्छी तरह से हो। उस रात भी वह अपने निरीक्षण के दौरे पर आयरन वर्क्स में आया था।)

Question 12.
How did the ironmaster react when he saw the ragged peddler? (जब उसने फटेहाल फेरी वाले को देखा तो आयरन मास्टर की क्या प्रतिक्रिया थी ?)
Answer:
After some time, the ironmaster, who owned the mill, came for his nightly inspection. He saw the peddler who was in rags. He mistook the peddler for an old acquaintance, Nils Olof. He wondered why his old friend was in rags. He invited him to visit his house and spend the night there.
(कुछ समय के पश्चात्, आयरन मास्टर, जो कि मिल का मालिक था, अपने रात्रि के समय के निरीक्षण के लिए आया। उसने फेरी वाले को देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसने गलती से उस फेरी वाले को अपना पुराना जान-पहचान वाला नील्स ओल्फ समझ लिया। वह हैरान था कि उसके पुराने मित्र ने चिथड़े क्यों पहन रखे थे। उसने उसे अपने घर आमंत्रित किया और उनके साथ रात बिताने के लिए कहा।)
Question 13.
Why was the peddler surprised when the ironmaster referred to him as his old friend? Why did he refuse to go with him.? ।
(जब आयरन मास्टर ने उसे अपना पुराना मित्र कहा तो फेरी वाला हैरान क्यों हो गया ? उसने उसके साथ जाने से इन्कार क्यों किया ?)
Answer:
The peddler had never seen the ironmaster before. Nor did he know his name. But he told the ironmaster that he was running into bad luck. The ironmaster told him that he should not have resigned from the regiment. Then the ironmaster invited him to his house for the Christmas Eve. But the peddler did not want to fall into any fresh trouble. So he emphatically refused to go with him.
(फेरी वाले ने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था। वह उसका नाम भी नहीं जानता था। लेकिन उसने आयरन मास्टर को बताया कि आजकल उसकी किस्मत खराब चल रही है। आयरन मास्टर ने उसको बताया कि उसे सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। तब आयरन मास्टर ने उसको क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने घर आमंत्रित किया। लेकिन फेरी वाला किसी नए संकट में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए उसने जोर देकर उसके साथ जाने से मना कर दिया।)
Question 14.
At last the peddler agreed to go to the ironmaster’s house and spend the night there. Why? (अन्त में फेरी वाला आयरन मास्टर के साथ जाने और वहाँ रात बिताने के लिए राजी हो गया। क्यों ?)
Answer:
The ironmaster had a young daughter named Edla. He thought that his daughter might persuade his old friend to stay with them. So he went home and brought his daughter. Edla looked at him compassionate. She requested him to come to her home. At last, the rattrap seller agreed and went with them.
(आयरन मास्टर की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम एडला था। वह सोचता था कि उसकी बेटी उसके पुराने मित्र को उनके साथ रात बिताने के लिए मना सकती थी। इसलिए वह घर गया और अपनी बेटी को लेकर आया। एडला ने उसकी ओर दया भाव से देखा। उसने उससे अपने घर आने की प्रार्थना की। अंत में, चूहेदानियों की फेरी वाला सहमत हो गया और उनके साथ चलागया।)
Question 15.
When did the ironmaster realise that the peddler was not his old friend? (आयरन मास्टर को ऐसा कब महसूस हुआ कि फेरी वाला उसका पुराना मित्र नहीं है ?)
Answer:
The next day was Christmas. The servant had bathed the peddler, cut his hair and shaved him. When the ironmaster came into the dining room he looked at him in broad daylight. Now he realised that he had been mistaken and that man was not his old friend.
(अगले दिन क्रिसमस था। नौकर ने फेरी वाले को स्नान करवा दिया था, उसके बाल काट दिए थे और दाढ़ी बना दी थी। जब आयरन मास्टर भोजन कक्ष में आया और दिन के प्रकाश में उसने उसे देखा। तब उसको उस बात का एहसास हो गया कि उससे गलती हो गई है और वह उसका पुराना मित्र नहीं है।)
Question 16.
What happened when the ironmaster realised his mistake? (जब आयरन मास्टर को अपनी भूल का एहसास हुआ तो क्या हुआ ?)
Answer:
The iron master realised that the peddler was not his old friend. He thundered at him and asked him who he was. He threatened to call the sheriff. But the peddler said that it was not his fault. He had not tried to deceive anybody. At this the ironmaster asked him to go away.
(आयरन मास्टर को इस बात का एहसास हो गया था कि फेरी वाला उसका पुराना मित्र नहीं है। वह उस पर गरजा और पूछा कि वह कौन है। उसने शेरिफ को बुलाने की धमकी दी। लेकिन फेरी वाले ने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने किसी को भी धोखा देने का प्रयास नहीं किया था। इस पर आयरन मास्टर ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा।)
Question 17.
Why didn’t the stranger tell the ironmaster that he was not Nils Ol of ? (अजनबी ने आयरन मास्टर को यह क्यों नहीं बताया कि वह निल्स ओलोफ नहीं था?) [H.B.S.E. 2019 (Set-A)]
Answer:
When the ironmaster came for his nightly inspection he saw a stranger (peddler) who was in rags. He mistook him for an old acquaintance, Nils Olof. He wondered why his old friend was in rags. He invited him to visit his house and spend the night there. But the stranger (peddler) did not tell him that he was not Nils Olof because he wanted shelter and food from him.
(जब रात को आयरन मास्टर निरीक्षण के लिए निकला तब उसने एक अजनबी (फेरी वाला) को देखा जो फटे पुराने कपड़ों में था। उसने गलती से उस अजनबी को अपना पुराना मित्र निल्स ओलोफ समझ लिया। परन्तु अजनबी ने उसे यह नहीं बताया कि वह उसका मित्र निल्स ओलोफ नहीं हैं क्योंकि आयरन मास्टर से उसे खाना और आसरा चाहिए था।)

Question 18.
What news did the ironmaster and his daughter hear at the church? What did the ironmaster fear?
(चर्च में आयरन मास्टर एवं उसकी बेटी ने क्या समाचार सुना ? आयरन मास्टर को क्या भय था ?)
Answer:
The next morning, the ironmaster and his daughter went to church for Christmas service. The seller was still as the ironmaster and his daughter came to know that one of the old crofters had been robbed by a man who sold rattraps. That news made Edla sad. Her father was afraid that the rattrap seller might have stolen all their silver spoons in their absence.
(अगली सुबह, आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस मनाने चर्च चले गए। चूहेदानियाँ बेचने वाला अभी भी सो रहा था। चर्च में आयरन मास्टर और उसकी बेटी को इस बात का पता चला कि एक बूढ़े किसान को एक आदमी ने लूट लिया है जो चूहेदानियाँ बेचता है। इस समाचार से एडला निराश हो गई। उसके पिता को डर था कि चूहेदानियाँ बेचने वाला उनकी गैरहाजरी में उनके चाँदी के सारे चम्मच चुरा सकता था।)
Question 19.
What present did the peddler leave for Edla? What did he write in his letter to her? (फेरी वाला एडला के लिए क्या उपहार छोड़ गया ? उसने उसके लिए अपने पत्र में क्या लिखा ?)
Answer:
The valet told Edla that the peddler left a little package for her. She found a small rattrap in the package. Inside the package there were three ten-kronor notes and a letter. In his letter he thanked her for being so nice to him as if he was really a captain. He did not want her to be troubled with a thief on Christmas. He requested her to return the money to the old crofter. He wrote that the rattrap was a Christmas present to her.
_(नौकर ने एडला को बताया कि फेरी वाला उसके लिए एक छोटा पैकेट छोड़कर गया है। उस पैकेट के अन्दर एक छोटी चूहेदानी थी। पैकेट के अन्दर दस क्रॉनर के तीन नोट और एक पत्र था। अपने पत्र में उसने, उनके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद किया जैसे कि वह कैप्टन ही हो। वह नहीं चाहता था कि उसको क्रिसमस पर एक चोर के साथ रहने का कष्ट हो। उसने उससे प्रार्थना की कि वह उस धन को बूढ़े किसान को लौटा दे। उसने लिखा कि चूहेदानी उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार है।)
Long Answer Type Questions
Answer the following questions in about 80 words
Question 1.
Who was the poor peddler? Why did he think that the whole world was a rattrap? (गरीब फेरी वाला कौन था ? वह ऐसा क्यों सोचता था कि सारा संसार एक चूहेदानी है ?)
Answer:
The peddler was a poor man. He made small rattraps of wire. He wandered from place to place selling these rattraps. But he could not earn enough to make both ends meet. So he had to beg as well as resort to petty thefts. His clothes were in rags, his cheeks were sunken and he had often to remain hungry. His life was sad and monotonous. One day, while selling rattraps, an idea struck his mind. He thought that the whole world is also like a rattrap. In a rattrap, the rat is caught when he is attracted to the bait and tries to eat it. In the same way the world sets baits for people. These baits are riches, joys, shelter, food and clothing. When a person is tempted towards these baits, he is caught like a rat. Then there is no escape from the clutches of the world. The peddler thought that life had never been kind to him. This world was just like a rattrap to him. This idea amused him. He was able to philosophise his misery and poverty
(फेरी वाला एक गरीब आदमी था। वह तार के साथ छोटी चूहेदानियाँ बनाता था। वह इन चूहेदानियों को बेचने के लिए जगह-जगह घूमता फिरता था। लेकिन वह इतना धन नहीं कमा पाता था जिससे उसका गुजारा हो सके। इसलिए उसको भीख माँगनी पड़ती थी और छोटी-मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। उसके कपड़े चिथड़े थे, उसकी गालें चिपकी हुई थी और उसको प्रायः भूखा रहना पड़ता था। उसका जीवन उदासी और नीरसता से भरा हुआ था। एक दिन, चूहेदानियाँ बेचते समय उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि यह सारा संसार एक चूहेदानी के समान है। चूहेदानी में चूहा फंस जाता है जब वह खाने की ओर आकर्षित हो जाता है और उसे खाने का प्रयास करता है। इसी तरह से यह संसार भी लोगों के लिए प्रलोभन प्रस्तुत करता है। ये प्रलोभन हैं अमीरी, खुशियाँ, घर, भोजन और वस्त्र। जब कोई व्यक्ति इन प्रलोभनों की ओर आकर्षित होता है, तो वह एक चूहे की तरह फंस जाता है। तब इस संसार के चंगुल से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। फेरी वाला सोचता है कि यह संसार कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा है। यह संसार उसके लिए मात्र एक चूहेदानी के समान था। इस विचार से वह खुश हो गया। वह अपने कष्टों और गरीबी के बारे में दार्शनिकतापूर्ण विचार करने लगा।)
Question 2.
Describe the peddler’s stay with the old crofter. How did he respond to the old man’s kindness and hospitality? (फेरी वाले का बूढ़े किसान के पास ठहरने का वर्णन करो। उसने बूढ़े व्यक्ति की दयालुता एवं आतिथ्य का क्या बदला चुकाया ?)
Answer:
One dark evening, the peddler was walking along the road with great difficulty. He noticed a little grey cottage by the roadside. He knocked on the door, an old man welcomed him. He was a crofter without wife or child. The old man was happy to get someone to talk to in his loneliness. He fed the peddler and played a game of cards with him until bedtime. The old man told him that he had been a crofter at Ramsjö Ironworks. Now he earned his living by selling his cow’s milk. He said that the previous month he had received thirty kronors in payment. The old man showed him the money which he kept in a leather pouch hung on a nail in the window frame. The next morning both the men left the cottage at the same time. But half an hour later, the peddler came back to the house. He went to window, smashed a pane and got hold of the pouch. He took out the money and hung the pouch back in its place. Then he went his way.
(एक अंधेरी शाम को फेरी वाला बड़ी कठिनाई के साथ सड़क पर चला जा रहा था। उसने सड़क किनारे स्लेटी रंग का एक छोटा-सा घर देखा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया। वह एक किसान था जिसकी पत्नी अथवा बच्चा नहीं था। बूढ़ा आदमी अपने अकेलेपन में किसी को अपने साथ बातें करने के लिए पाकर प्रसन्न था। उसने फेरी वाले को भोजन कराया और रात को सोने के समय तक उसके साथ ताश खेली। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह रेमस्जो आयरन वर्क्स में एक किसान के रूप में काम कर चुका था। अब वह अपनी गाय का दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता था। उसने कहा कि पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में तीस क्रॉनर मिले थे। बूढ़े आदमी ने उसको वह धन दिखाया जो कि उसने एक चमड़े की थैली में डालकर खिड़की के पास कील पर टाँगा हुआ था। अगली सुबह दोनों आदमी एक साथ घर से बाहर गए। लेकिन आधे घंटे के पश्चात् फेरी वाला घर वापस लौटा। वह खिड़की के पास गया, एक शीशा तोड़ा और थैली को उतार लिया। उसने थैली से धन बाहर निकाला और थैली को वापस वहीं टाँग दिया। तब वह चला गया।)

Question 3.
Where did the peddler go after stealing the old crofter’s money? (बूढ़े किसान का पैसा चुराने के बाद फेरी वाला कहाँ गया ?)
Answer:
The old crofter treated the peddler in a kind manner. He offered him food and shelter for the night. He played a game of cards with him until bed time. But the peddler stole his money and went away. With the stolen money in his pocket, it was not safe for the peddler to walk on the public highway. So he turned off the road into a forest. Later in the day he got into a big and confusing forest. He walked and walked without coming to the end of the forest. Now he felt that the world was really a big rattrap.
The money he had stolen was the bait and he had been trapped. Darkness was descending. It was late in December and the forest was getting cold. When he had lost hope of survival, he heard a sound. It was the sound of hammer strokes coming from an iron mill. He got up and moved with difficulty towards the sound. The rattrap seller reached the Ramsjö Ironworks and entered it. The blacksmiths looked at him with indifference. He asked permission to stay there for the night which was granted by the chief blacksmith.
(बूढ़े किसान ने एक दयालु ढंग के साथ फेरी वाले के साथ व्यवहार किया। उसने उसे भोजन और रात को ठहरने के लिए आश्रय दिया। उसने उसके साथ सोने के समय तक ताश भी खेली। लेकिन फेरी वाले ने उसका धन चोरी कर लिया और वह चला गया। अपनी जेब में चोरी किया हुआ धन डालकर, फेरी वाले के लिए मुख्य मार्ग से होकर जाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए वह सड़क मार्ग छोड़कर जंगल के रास्ते से गया। बाद में वह एक बड़े और उलझन भरे जंगल में घुस गया। वह चलता गया, चलता गया लेकिन जंगल कहीं भी समाप्त नहीं हुआ। अब उसे महसूस हुआ कि यह संसार सचमुच में एक बड़ी चूहेदानी था। जो धन उसने चोरी किया था वह एक प्रलोभन था और वह उसमें फंस चुका था। अंधेरा घना होता जा रहा था।
दिसम्बर महीने के अंतिम दिन थे और जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी। जब उसने अपने जीवित रहने की आशा खो दी तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह हथौड़े के टकराने की आवाज थी जो कि एक लोहे के कारखाने से आ रही थी। वह उठ खड़ा हुआ और कठिनाई के साथ उस आवाज की ओर बढ़ा। चूहेदानी की फेरी लगाने वाला रेमस्जो आयरन वर्क्स पहुंचा और उसमें प्रवेश कर गया। लोहारों ने उसकी ओर उदासीनतापूर्वक देखा। उसने वहाँ रात को ठहरने के लिए अनुमति माँगी जो कि मुख्य लोहार के द्वारा प्रदान कर दी गई।)
Question 4.
Why did the peddler agree to spend the night at the house of the ironmaster? Why did the ironmaster ask him to go the next morning?
(फेरी वाला आयरन मास्टर के घर रात बिताने के लिए राजी क्यों हो गया ? अगली प्रातः आयरन मास्टर ने उसे चले जाने को क्यों कह दिया ?)
Answer:
The peddler was given permission to stay at the ironworks. After some time, the ironmaster came for his nightly inspection. He saw the peddler who was in rags. He mistook the peddler for an old acquaintance, Nils Olof. He wondered why his old friend was in rags. The peddler had never seen him. Nor did he know his name. But he told the ironmaster that he was running into bad luck. The ironmaster told him that he should not have resigned from the regiment.
Then the ironmaster invited him to his house for the Christmas Eve. But the peddler did not want to fall into any fresh trouble. So he emphatically refused to go with him. The ironmaster then asked his daughter Edla to persuade his old friend to stay with them. She requested him to come to her home. At last, the rattrap seller agreed and went with them. The next day was Christmas. The servant had bathed him, cut his hair and shaved him. When the ironmaster came into the dining room he looked at him in broad daylight. Now he realised that he had been mistaken and that man was not his old friend. He thundered at him and asked him to go away.
(फेरी वाले को आयरन वर्क्स में ठहरने की अनुमति प्रदान की गई। कुछ समय के पश्चात् आयरन मास्टर रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए आया। उसने फेरी वाले को देखा, जिसने फटे-पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसने फेरी वाले को गलती से अपना पुराना जान-पहचान वाला नील्स ओल्फ समझ लिया। वह हैरान था कि उसका पुराना मित्र चिथड़ों में क्यों था। फेरी वाले ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। न ही वह उसका नाम जानता था। लेकिन उसने आयरन मास्टर को बताया कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है।
आयरन मास्टर ने उसको बताया कि उसे सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। तब आयरन मास्टर ने उसको क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने घर आमंत्रित किया। लेकिन फेरी वाला किसी नए संकट में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए उसने बलपूर्वक ढंग से उनके साथ जाने से मना कर दिया। तब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला से कहा कि वह उसके पुराने मित्र को उनके साथ ठहरने के लिए मना ले। उसने उससे अपने घर आने के लिए प्रार्थना की। अंततः चूहेदानियाँ बेचने वाला मान गया और उनके साथ चला गया। अगले दिन क्रिसमस था। नौकर ने उसे स्नान करा दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसकी दाढ़ी बना दी थी। जब आयरन मास्टर भोजन कक्ष में आया तो उसने दिन के प्रकाश में उसे देखा। अब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसे गलती लग गई है। वह उस पर गरजा और उसे चले जाने के लिए कहा।)
Question 5.
Why did the ironmaster’s daughter insist that the peddler should stay with them? What happened in the end? (आयरन मास्टर की बेटी ने इस बात का आग्रह क्यों किया कि फेरी वाला उनके साथ रहे ? अन्त में क्या हुआ?) Or How did the peddler show his gratitude to Edla? (फेरी वाले ने एडला को अपनी कृतज्ञता कैसे दिखाई?) [H.B.S.E. March, 2018 (Set-D)]
Answer:
The ironmaster asked the peddler to go away. But his daughter Edla wanted the peddler to stay with them that day. She said that they let him stay and enjoy a day of peace. They should not chase away a man whom they had promised invitation to enjoy the Christmas joy. Then she asked him to sit down and eat. The next morning the ironmaster and his daughter went to church for Christmas service.
The rattrap seller was still asleep. At church the ironmaster and his daughter came to know that one of the old crofters had been robbed by a man who sold rattraps. That news made Edla sad. Her father was afraid that the rattrap seller might have stolen all their silver spoons in their absence. But the valet told them that the peddler had not taken anything with him. Rather he had left a little package for the girl. She found a small rattrap in the package. Inside the package there were three ten-kronor notes and a letter. In his letter he thanked her for being so nice to him as if he was really a captain. He did not want her to be troubled with a thief on Christmas. He requested her to return the money to the old crofter. He wrote that the rattrap was a Christmas present to her.
(आयरन मास्टर ने फेरी वाले से चले जाने को कहा। लेकिन उसकी बेटी एडला चाहती थी कि वह उस रात को उनके साथ ठहरे। उसने कहा कि उन्होंने उसे एक दिन उनके साथ चैन से रहने की अनुमति प्रदान की थी। उन्हें उस आदमी को भगाना नहीं चाहिए जिसको कि उन्होंने क्रिसमस की खुशियों के लिए निमंत्रण का वायदा किया था। तब उसने उससे कहा कि वह बैठ जाए और खाना खाए। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में क्रिसमस मनाने चले गए। चूहेदानियाँ बेचने वाला अभी भी सो रहा था।
चर्च में आयरन मास्टर और उसकी बेटी को जानकारी मिली कि एक बूढ़े किसान को एक चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी ने ठग लिया है। इस समाचार ने एडला को उदास कर दिया। उसके पिता को डर लग रहा था कि चूहेदानियाँ बेचने वाला उनकी गैर हाजरी में उनके चाँदी के सारे चम्मच चुरा सकता था। लेकिन नौकर ने उन्हें बताया कि फेरी वाला अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। बल्कि वह लड़की के लिए एक छोटा-सा पैकेट छोड़कर गया है। उसने पैकेट के अन्दर एक छोटी-सी चूहेदानी को पाया। उस पैकेट के अन्दर दस क्रॉनर के तीन नोट और एक पत्र भी था। अपने पत्र में उसने उस लड़की का अपने प्रति इतना अच्छा व्यवहार करने जैसे कि वह एक कैप्टन हो; के लिए धन्यवाद किया। वह नहीं चाहता था कि उसे क्रिसमस के अवसर पर एक चोर के साथ रहने का कष्ट हो। उसने उससे प्रार्थना की कि वह उस धन को बूढ़े किसान को लौटा दे। उसने लिखा कि चूहेदानी उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार थी।)

Question 6.
Do you think that the peddler is a criminal or a victim of circumstances? (आपके विचार में फेरी वाला अपराधी है या परिस्थितियों का शिकार है ?) [H.B.S.E. 2017 (Set-A)]
Or
Write a brief character-sketch of the peddler. (फेरी वाले का संक्षिप्त चरित्र-चित्रण करो।)
Answer:
The rattrap seller is a very poor man. He goes from place to place selling rattraps. But he does not earn enough to keep his body and soul together. So he resorts to begging and petty thefts. We know that stealing is a crime. Yet we do not hate him. We have sympathy for him. We know that he is not a habitual thief. If he had been a habitual thief, he would have committed big thefts and there would have been no need for him to wander here and there selling rattraps. He commits thefts only when he has nothing to eat. Although he is a poor, he is a thinker. He can philosophise about his condition. He steals the money of the old crofter. But the feeling of guilt remains with him. When Edla shows love and sympathy to him, he repents at his deed. His goodness is awakened. He leaves the money and requests Edla to return it to the old man. Thus we find that the poor rattrap peddler is not a criminal. He is only a victim of circumstances.
(चूहेदानियाँ बेचने वाला एक अति गरीब आदमी है। वह चूहेदानियाँ बेचने के लिए जगह-जगह जाता है। लेकिन वह इतना धन भी नहीं कमा पाता है कि अपने आप को जीवित रख सके। इसलिए वह भीख माँगने और छोटी-मोटी चोरियाँ करने लग जाता है। हम जानते हैं कि चोरी करना एक अपराध है। फिर भी हम उससे घृणा नहीं करते हैं। हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। हम जानते हैं कि वह एक पक्का चोर नहीं है। यदि वह एक पक्का चोर होता तो फिर वह बड़ी चोरियाँ करता और उसको इधर-उधर घूम कर चूहेदानियाँ बेचने की भी जरूरत न पड़ती। वह तभी चोरी करता है जब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। यद्यपि वह एक गरीब है लेकिन वह एक विचारक है। वह अपनी स्थिति पर दार्शनिकतापूर्ण विचार कर सकता है। वह बूढ़े किसान का धन चोरी कर लेता है। लेकिन अपराध बोध की भावना उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जब एडला उसके प्रति प्यार और सहानुभूति दिखाती है, तो उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। उसकी अच्छाई जागृत हो जाती है। वह धन वहीं छोड़ जाता है और एडला से प्रार्थना करता है कि वह उसे बूढ़े आदमी को लौटा दे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गरीब चूहेदानियाँ बेचने वाला फेरी वाला एक अपराधी नहीं है। वह तो केवल परिस्थितियों का मारा हुआ है।)
The Rattrap MCQ Questions with Answers
1. Who is the writer of the story ‘The Rattrap’?
(A) Ruskin Bond
(B) Selma Lagerlof
(C) R.K. Narayan
(D) Tagore
Answer:
(B) Selma Lagerlof
2. Who is the main character in the story “The Rattrap’?
(A) a poor man who made rattraps
(B) a rich man
(C) a doctor
(D) a teacher
Answer:
(A) a poor man who made rattraps
3. The poor man in the story could not make enough money by selling rattraps. What else did he do in order to make both ends meet?
(A) worked as a laborer
(B) did part-time work as a teacher
(C) did farming
(D) begged and stole
Answer:
(D) begged and stole
4. What idea struck the rattrap seller’s mind one day?
(A) this world is joyful and wonderful
(B) he should run away
(C) the whole world is also like a rattrap
(D) people are wonderful
Answer:
(C) the whole world is also like a rattrap
5. What did the rattrap seller notice one dark evening, as he was walking along the road?
(A) a big car
(B) a little grey cottage
(C) a big house
(D) a beautiful woman
Answer:
(B) a little grey cottage

6. Who was the old man living in the little cottage?
(A) an engineer
(B) a politician
(C) a crofter without wife or children
(D) a thief
Answer:
(C) a crofter without wife or children
7. What did the old man do for a living?
(A) selling his cow’s milk
(B) he begged
(C) he was a farmer
(D) he wrote poems
Answer:
(A) selling his cow’s milk
8. Where did the old man keep his money?
(A) in a chest
(B) in his box
(C) in the bank
(D) in a leather pouch
Answer:
(D) in a leather pouch
9. Who stole the old man’s money?
(A) his neighbour
(B) his son
(C) the rattrap seller
(D) his wife
Answer:
(C) the rattrap seller
10. How did the rattrap seller enter the cottage in order to steal the old man’s money?
(A) by breaking the lock
(B) by smashing a window pane
(C) by breaking the door
(D) by entering through the ventilator
Answer:
(B) by smashing a window pane
11. What happened when the rattrap seller left the main road and went into a forest?
(A) he was happy there
(B) he took rest there
(C) he enjoyed the forest
(D) he became confused and lost the way
Answer:
(D) he became confused and lost the way
12. When the rattrap seller had lost all hope, he heard a sound. From where was the sound coming?
(A) from a school
(B) from a mill
(C) from a lake
(D) from a shop
Answer:
(B) from a mill
13. Where did the rattrap seller reach when he followed the sound?
(A) a school
(B) a shop
(C) a hill
(D) the Ramsjo Ironworks
Answer:
(D) the Ramsjo Ironworks.

14. For what did the rattrap seller ask permission?
(A) to stay there for the night
(B) to dance in the factory
(C) to help the blacksmiths
(D) to build a wall
Answer:
(A) to stay there for the night
15. What did the owner of the factory mistake the rattrap seller for?
(A) a police inspector
(B) his old friend Nils Ol of
(C) a soldier
(D) a teacher
Answer:
(B) his old friend Nils Olof
16. Where did the ironmaster invite the rattrap seller?
(A) to the dance party
(B) to the hospital
(C) to his house for the Christmas Eve
(D) to a marriage party
Answer:
(C) to his house for the Christmas Eve
17. What was the name of the ironmaster’s daughter?
(A) Edla
(B) Pedal
(C) Sedla
(D) Media
Answer:
(A) Edla
18. At first the rattrap seller declined the ironmaster’s invitation. But then why did he agree to go to his house as his guest?
(A) because he was hungry
(B) because he wanted to sleep
(C) because the ironmaster’s daughter invited him
(D) because he wanted to steal ironmaster’s money
Answer:
(C) because the ironmaster’s daughter invited him
19. What happened when the ironmaster saw the rattrap seller looked at him in broad day light?
(A) he praised the personality of the rattrap seller
(B) he gave him good food
(C) he embraced him
(D) he recognized that he was not his friend
Answer:
(D) he recognized that he was not his friend
20. When the ironmaster asked the peddler to go away, what did his daughter say?
(A) she asked the peddler to stay with them that day
(B) she abused the peddler
(C) she beat the peddler
(D) she reported him to the police
Answer:
(A) she asked the peddler to stay with them that day
21. At the church next day, what did the ironmaster and his daughter come to know about the rattrap seller?
(A) that he was a rich man
(B) that he had stolen the old crofter’s money
(C) that the rattrap seller had run away
(D) that he had been arrested
Answer:
(B) that he had stolen the old crofter’s money
22. What did ironmaster feel when he learnt that the rattrap seller was a thief?
(A) that the rattrap seller might steal his silver spoons
(B) that he should report the matter to the police
(C) that he should beat the man
(D) that he should shoot him down
Answer:
(A) that the rattrap seller might steal his silver spoons.

23. What had the rattrap seller left for the ironmaster’s daughter as a Christmas gift?
(A) a silver ring
(B) a gold ring
(C) a beautiful dress
(D) the rattrap
Answer:
(D) the rattrap
The Rattrap Important Passages for Comprehension
Seen Comprehension Passages
Read the following passages and answer the questions given below:
Type (i)
Passage 1
One dark evening as he was trudging along the road he caught sight of a little gray cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper; then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger’s pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played ‘majlis’ with his guest until bedtime. [H.B.S.E. 2019 (Set-D)]
Word-meanings :
Trudging = wandering (आवारागर्दी);
sour = unpleasant (अप्रिय);
porridge = oat meal (दलिया)।
Questions :
(i) Name the chapter from which these lines have been taken?
(A) The Last Lesson
(B) Lost Spring
(C) Deep Water
(D) The Rattrap
Answer:
(D) The Rattrap
(ii) Name the writer of this passage.
(A) Alphonse Daudet
(B) Anees Jung
(C) William O Douglas
(D) Selma Lagerl of
Answer:
(D) Selma Lagerlöf
(iii) What did the vagabond see one dark evening?
(A) a little gray cottage
(B) an old woman
(C) a small boy
(D) all the above
Answer:
(A) a little gray cottage
(iv) Who was the owner of the cottage?
(A) an old woman
(B) an old man
(C) a rattrap seller
(D) the author himself
Answer:
(B) an old man
(v) Who were these two men?
(A) The old man and his guest
(B) The old man and his son
(C) The old man and his wife
(D) The old man and his father
Answer:
(A) The old man and his guest
Passage 2
The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rattraps said good bye and thank you, and thereupon each went his own way.
But half an hour later the rattrap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the thirty kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away.
Word-meanings :
Probably = perhaps (शायद);
smashed = broke (तोड़ा) ।
Questions :
(i) Name the chapter from which these lines have been taken?
(A) The Last Lesson
(B) Lost Spring
(C) Deep Water
(D) The Rattrap
Answer:
(D) The Rattrap
(ii) Name the writer of this passage.
(A) Alphonse Daudet
(B) Anees Jung
(C) William O Douglas
(D) Selma Lagerl of
Answer:
(D) Selma Lagerl of
(iii) Who was in a hurry?
(A) The Crofter
(B) The other man
(C) Both (A) and (B)
(D) none of the above
Answer:
(A) The Crofter.

(iv) What did the rattrap peddler do after half an hour?
(A) He went back to him home
(B) He came back to the old man’s cottage
(C) He went to the market to sell rattraps
(D) none of the above
Answer:
(B) He came back to the old man’s cottage
(v) What did he steal from the old man’s cottage?
(A) Rattraps
(B) Watch
(C) Money
(D) Food
Answer:
(C) Money
Passage 3
It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound a hard regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. “Those are the hammer strokes from an iron mill”, he thought. “There must be people nearby”. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound.
Word-meanings :
Descending = coming down (नीचे आते हुए);
gloom = sadness (उदासी)।
Questions :
(i) Name the chapter from which these lines have been taken?
(A) The Last Lesson
(B) Lost Spring
(C) Deep Water
(D) The Rattrap
Answer:
(D) The Rattrap
(ii) Name the writer of this passage.
(A) Alphonse Daudet
(B) Anees Jung
(C) William O Douglas
(D) Selma Lagerl of
Answer:
(D) Selma Lagerlöf
(iii) What increased the rattrap seller’s despair?
(A) darkness and cold
(B) hunger and weakness
(C) disease and old age
(D) all the above
Answer:
(A) darkness and cold
(iv) What did he hear when he laid his head to the ground?
(A) hissing sounds
(B) humming sound
(C) creaking sounds
(D) chirping sounds
Answer:
(B) humming sound
(v) Where did he go after summoning his strength?
(A) in the direction of the sound
(B) to him home
(C) to the old man’s home
(D) none of the above
Answer:
(A) in the direction of the sound
Passage 4
During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes.
[H.B.S.E. 2017 (Set-B)]
All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof.
Word-meanings :
Glowing = shining (चमकना);
shoveled = put through shovels (फावड़े से डालना)।
Questions :
(i) Name the chapter from which these lines have been taken?
(A) The Last Lesson
(B) Lost Spring
(C) Deep Water
(D) The Rattrap
Answer:
(D) The Rattrap
(ii) Name the writer of this passage.
(A) Alphonse Daudet
(B) Anees Jung
(C) William O Douglas
(D) Selma Lagerl of
Answer:
(D) Selma Lagerl of
(iii) Who sat in the dark forge near the furnace?
(A) the master smith
(B) his helper
(C) both (A) and (B)
(D) none of the above
Answer:
(C) both (A) and (B)
(iv) What sounds were coming from the furnace?
(A) groaning of bellowing
(B) cracking of coal
(C) both (A) and (B)
(D) none of the above
Answer:
(C) both (A) and (B)

(v) What was he wearing?
(A) a short shirt and a pair of wooden shoes
(B) a long shirt and a pair of wooden shoes
(C) a long shirt and a pair of leather shoes
(D) a short shirt and a pair of leather shoes
Answer:
(B) a long shirt and a pair of wooden shoes
Type (ii)
Passage 5
No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought, which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rattraps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him – the whole world with its lands and seas, its cities and villages – was nothing but a big rattrap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rattrap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end.
Word-meanings :
Vagabond = wanderer (आवारा);
rattrap = a device for catching rats (चूहेदानी)।
Questions :
(i) Name the lesson and its author.
(ii) How does life appear to a vagabond?
(iii) What is the routine of a vagabond?
(iv) What did the vagabond sell in the passage?
(v) Find words from the passage which mean the same as :
(a) wandered, (b) a device for catching rats.
Answers:
(i) Chapter : The Rattrap.
Author : Selma Lagerlof.
(ii) Life appears sad and monotonous to a vagabond.
(iii) A vagabond plods along the road, left to his own meditations.
(iv) The vagabond sold the rattraps in the passage.
(v) (a) vagabond, (b) rattrap.
Passage 6
The man with the rattraps had never before seen the ironmaster at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor. Therefore he did not want to undeceive him all at once.
“Yes, God knows things have gone downhill with me”, he said. “You should not have resigned from the regiment”, said the ironmaster. “That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me,”
Word-meanings :
Acquaintance = a known person (परिचित);
regiment = mathrm unit of army (सेना दल)।
Questions :
(i) Name the chapter and its author.
(ii) Why did the rattrap peddler not want to undeceive the ironmaster?
(iii) What did the ironmaster think the rattrap peddler to be?
(iv) What did the rattrap peddler not want to do all at once?
(v) Find words from the passage having the meaning same as :
(a) a known person, (b) thought appeared in brain.
Answers:
(i) Chapter: The Rattrap.
Author: Selma Lagerlof.
(ii) The rattrap peddler did not want to undeceive the iron master because he wanted shelter and food from him.
(iii) He thought him an old acquaintance of him.
(iv) He did not want to undeceive the ironmaster all at once.
(v) (a) acquaintance, (b) occurred.
Passage 7
The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. “First of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones,” he said to his daughter, who was busy at the table. “And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rattraps.”
“It is queer that things have gone downhill with him as badly as that,” said the daughter. “Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man.”
Word-meanings :
Comrade = friend (साथी);
queer= strange (अजीब)।
Questions :
(i) Name the chapter and its author.
(ii) What special occasion was the next day?
(iii) Why did the ironmaster visit the dining room?
(iv) What did the ironmaster’s daughter think about the rattrap peddler?
(v) Find words from the passage having the meaning same as :
(a) friend, (b) strange.
Answers :
(i) Chapter: The Rattrap.
Author: Selma Lagerlof.
(ii) The next day it was the christmas Eve.
(iii) He visited the dining room for breakfast.
(iv) She thought the rattrap peddler as an unlucky man.
(v) (a) comrade, (b) queer.
Passage 8
But half an hour later, the rattrap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the thirty kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch carefully back in its place and went away. [H.B.S.E. March 2018 (Set-D)]
Word-meanings :
Smashed = broke (तोड़ा);
pane = window glass (खिड़की का शीशा);
thrust = pushed (डालना)।
Questions :
(i) Name the chapter from which the above lines have been taken.
(ii) Name the author of the chapter.
(iii) Why did the rattrap peddler not try to get in?
(iv) Where had the leather pouch been hanging?
(v) What was there in the leather pouch?
Answers :
(i) The Rattrap
(ii) Selma Lagerlof
(iii) The rattrap peddler did not try to get in because he knew where the money pouch was.
(iv) The leather pouch was hanging near the window.
(v) There were thirty kroner in the leather pouch.
The Rattrap Summary in English and Hindi
The Rattrap Introduction to the Chapter
Selma Lagerlöf was a Swedish writer. She worked as a country school teacher for nearly ten years before adopted writing as her career. The particular focus of her stories and novels was on the legends she had learned as a child. In 1909 she was awarded the Nobel prize for literature. She was the first woman to get this prize for literature. “The Rattrap’ is an interesting story. It has been told somewhat in the manner of a fairy tale. The rattrap peddler is a poor man. He robs the same who gives him shelter and food. But he is reformed by the compassionate behaviour of a young girl Edla. The story gives the message that the essential goodness of man can be awakened through love and understanding.
(Selma Lagerlöf एक स्वीडिश लेखिका थी। लेखन के रूप में अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले उसने लगभग दस साल तक एक ग्रामीण स्कूल में काम किया था। उनकी कहानियों और उपन्यासों का विशेष केंद्र उन दंत कथाओं पर था जो बचपन में उसने सीखी थीं। 1909 में उनको साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह प्रथम महिला थी। ‘The Rattrap’ एक रोचक कहानी है। यह कुछ-कुछ परियों की कहानी के रूप में सुनाई गई है। चूहेदानियाँ बेचने वाला व्यक्ति एक गरीब आदमी है। वह उसी को ठगता है जो उसे आश्रय और भोजन प्रदान करता है। लेकिन एक छोटी लड़की एडला का दयालुतापूर्ण व्यवहार उसे परिवर्तित कर देता है। कहानी संदेश देती है कि मनुष्य की जरूरी अच्छाई को प्यार और समझ के द्वारा जगाया जा सकता है।)
The Rattrap Summary
This story is about a poor man who made small rattraps of wire. He wandered from place to place selling these rattraps. But he could not earn enough to make both ends meet. So he had to beg as well as resort to petty thefts. His clothes were in rags, his cheeks were sunken and he had often to remain hungry. His life was sad and monotonous.
One day, while selling rattraps, an idea struck his mind. He thought that the whole world is also like a rattrap. In a rattrap, the rat is caught when he is attracted to the bait then he tries to eat it. In the same way the world sets baits for people. These baits are riches, joys, shelter, food and clothing. When a person is tempted towards these baits, he is caught like a rat. The peddler thought that life had never been kind to him. This world was just like a rattrap to him.

One dark evening, he was walking along the road with great difficulty. He noticed a little grey cottage by the roadside. He knocked on the door, an old man welcomed him. He was a crofter without wife or children. The old man was happy to get someone to talk to in his loneliness. He fed the peddler and played a game of cards with him until bedtime. The old man told him that he had been a crofter at Ramsjö Ironworks. Now he earned his living by selling his cow’s milk. He said that the previous month he had received thirty kronors in payment. The old man showed him the money which he kept in a leather pouch hung on a nail in the window frame.
The next morning both the men left the cottage at the same time. But half an hour later, the peddler came back to the house. He went to window, smashed a pane and got hold of the pouch. He took out the money and hung the pouch back in its place. Then he went his way.
With the stolen money in his pocket, it was not safe for the peddler to walk on the public highway. So he turned off the road into a forest. Later in the day he got into a big and confusing forest. He walked and walked without coming to the end of the forest. Now he felt that the world was really a big rattrap. The money
he had stolen was the bait and he had been trapped. Darkness was descending. It was late in December and the forest was getting cold. When he had lost hope of survival, he heard a sound. It was the sound of hammer strokes coming from a iron mill. He got up and moved with difficulty towards the sound.
The rattrap seller reached the Ramsjö Ironworks and entered it. The blacksmiths looked at him with indifference. He asked permission to stay there for the night which was granted by the chief blacksmith. After some time, the ironmaster, who owned the mill, came for his nightly inspection. He saw the peddler who was in rags. He mistook the peddler for an old acquaintance, Nils Olof.
He wondered why his old friend was in rags. The peddler had never seen him. Nor did he know his name. But he told the ironmaster that he was running into bad luck. The ironmaster told him that he should not have resigned from the regiment. Then the ironmaster invited him to his house for the Christmas Eve. But the peddler did not want to fall into any fresh trouble. So he emphatically refused to go with him.
The ironmaster had a young daughter named Edla. He thought that his daughter might persuade his old friend to stay with them. So he went home and brought his daughter. Edla looked at him compassionately. She requested him to come to her home. At last, the rattrap seller agreed and went with them. The next day was Christmas. The servant had bathed him, cut his hair and shaved him. When the ironmaster came into the dining room he looked at him in broad daylight. Now he realised that he had been mistaken and that man was not his old friend. He thundered at him and asked him who he was.
He threatened to call the sheriff. But the peddler said that it was not his fault. He had not tried to deceive anybody. At this the ironmaster asked him to go away. But the ironmaster’s daughter wanted the peddler to stay with them that day. She said that they let him stay and enjoy a day of peace. They should not chase away a man whom they had promised invited to enjoy the Christmas joy. Then she asked him to sit down and eat. In the evening the Christmas tree was lighted. He thanked everybody.
The next morning the ironmaster and his daughter went to church for Christmas service. The rattrap seller was still asleep. At church the ironmaster and his daughter came to know that one of the old crofters had been robbed by a man who sold rattraps. That news made Edla sad. Her father was afraid that the rattrap seller might have stolen all their silver spoons in their absence. But the valet told them that the peddler had not taken anything with him. Rather he had left a little package for the girl.
She found a small rattrap in the package. Inside the package there were three ten-kronor notes and a letter. In his letter he thanked her for being so nice to him as if he was really a captain. He did not want her to be troubled with a thief on Christmas. He requested her to return the money to the old crofter. He wrote that the rattrap was a Christmas present to her.
(यह कहानी एक गरीब आदमी के बारे में है जो तार की छोटी चूहेदानियाँ बनाया करता था। वह इन चूहेदानियों को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। लेकिन वह अपना गुजारा चलाने जितना भी नहीं कमा सकता था। इसलिए उसे या तो भीख माँगनी पड़ती थी या फिर छोटी-मोटी चोरियाँ करनी पड़ती थीं। उसके कपड़े चिथड़े थे, उसकी गालें धंसी हुई थीं और उसे हमेशा भूखा रहना पड़ता था। उसका जीवन उदास और नीरस था।
एक दिन, चूहेदानियाँ बेचते समय, उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि सारा संसार ही एक चूहेदानी के समान है। चूहेदानी में चूहा पकड़ा जाता है जब वह फँसाने के सामान (रोटी) की ओर आकर्षित होता है तो वह उसे खाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से संसार लोगों के लिए फंदे लगाता है। ये फंदे हैं, अमीरी, आनंद, आश्रय, भोजन और वस्त्र । जब एक व्यक्ति इन साधनों की लालसा करता है, तो वह चूहे की भाँति फँस जाता है। फेरी वाले ने सोचा कि जीवन कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा है। यह संसार तो उसके लिए केवल चूहेदानी के समान था।
एक अंधेरी शाम को, वह बड़ी कठिनाई के साथ सड़क के साथ-साथ चल रहा था। उसने सड़क के किनारे स्लेटी रंग के एक छोटे से घर को देखा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया। वह बिना पत्नी और बच्चों के एक छोटा-सा किसान था। वृद्ध आदमी अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए पाकर खुश था। उसने फेरी वाले को भोजन खिलाया और रात्रि को सोने के समय तक उसके साथ ताश खेले। वृद्ध आदमी ने उसे बताया कि वह रेमस्जो लौह मिल में एक छोटे किसान के रूप में कार्य करता था। अब वह अपनी गाय का दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता था। उसने कहा कि पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में तीस क्रॉनर प्राप्त हुए थे। वृद्ध आदमी ने उसे वह धन दिखाया जो उसने चमड़े की एक थैली में रखा था जो कि खिड़की के फ्रेम में लटक रही थी।
अगली सुबह दोनों आदमी एक-साथ घर से बाहर चले गए। लेकिन आधे घंटे के पश्चात्, फेरी वाला घर में वापिस आया। वह खिड़की के पास गया, एक काँच को तोड़ा और छोटी थैली हासिल कर ली उसने धन बाहर निकाला और थैली को वापिस उसी स्थान पर टाँग दिया। तब वह अपने रास्ते चला गया। अपनी जेब में चोरी किए हुए धन के साथ, फेरी वाले के लिए आम जनता वाली सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं था। इसलिए वह सड़क मार्ग से हटकर जंगल के मार्ग की ओर गया। बाद में दिन में वह एक बड़े और उलझन भरे जंगल में फँस गया। वह चलता गया लेकिन जंगल का कोई सिरा नहीं आया। अब उसने महसूस किया कि दुनिया वास्तव में ही एक बड़ी चूहेदानी थी। धन जो उसने चोरी किया था एक फँसाने वाली चीज़ थी और वह उसमें फँस चुका था। अंधेरा होता जा रहा था। दिसंबर के आखिरी दिनों की बात थी और जंगल में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जब उसने बचने की उम्मीद खो दी, उसने एक आवाज़ सुनी। यह एक लोहे के कारखाने से आ रही थी। यह एक घन (हथौड़ा) के प्रहार की आवाज थी। वह उठ खड़ा हुआ और कठिनाई के साथ आवाज की दिशा में चल पड़ा।

फेरी वाला रेमस्जो लौह मिल में पहुँचा और उसमें प्रवेश कर गया। लोहार ने लापरवाहीपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखा। उसने वहाँ रात्रि को ठहरने की अनुमति माँगी जो कि मुख्य लोहार के द्वारा प्रदान कर दी गई। कुछ समय के पश्चात्, लोहार जो कि मिल का मालिक था, अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए आया। उसने फेरी वाले को देखा जिसके वस्त्र फटे-पुराने थे। उसने गलती से फेरी वाले को अपना पुराना परिचित नील्स ऑलोफ समझ लिया। वह हैरान था कि उसका पुराना मित्र चिथड़ों में क्यों था। फेरी वाले ने उसे कभी नहीं देखा था। न ही वह उसका नाम जानता था। लेकिन उसने लोहार को बताया कि उसकी किस्मत खराब चल रही है। लोहार ने उसे बताया कि उसे सेना की टुकड़ी से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। तब लोहार ने उसे ‘क्रिसमस की पूर्व संध्या’ पर अपने घर आमंत्रित कर लिया। लेकिन फेरी वाला किसी नए संकट में फँसना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उसके साथ जाने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया।
लोहार की एक युवा बेटी थी जिसका नाम एडला था। उसने सोचा कि उसकी बेटी उसके पुराने मित्र को उसके साथ ठहरने के लिए मना लेगी। इसलिए वह घर गया और अपनी बेटी को लेकर आया। एडला ने उसकी ओर दयाभाव के साथ देखा। उसने उससे निवेदन किया कि वह उसके घर आए। अंततः चूहेदानी बेचने वाला सहमत हो गया और उनके साथ चल दिया। अगले दिन क्रिसमस था। नौकर ने उसे स्नान करा दिया था, उसके बाल काट दिए थे और दाढ़ी बना दी थी। जब लोहार भोजन-कक्ष में आया, उसने दिन के प्रकाश में उसकी ओर देखा। अब उसने महसूस किया कि उससे गलती हो गई थी और वह आदमी उसका पुराना मित्र नहीं था। वह उस पर गरजा और उससे पूछा कि वह कौन है। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। लेकिन फेरी वाले ने कहा कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने किसी को भी धोखा देने का प्रयास नहीं किया था। इस पर लोहार ने उसे चले जाने को कहा।
लेकिन लोहार की बेटी चाहती थी कि वह फेरी वाला उस दिन उनके पास ही ठहर जाए। उसने कहा कि उन्होंने उसे एक दिन रहने और सकून का आनंद लेने की अनुमति दी थी। उन्होंने क्रिसमस का आनंद मनाने के लिए वादा किया था। उनको क्रिसमस की खुशियों का आनंद उठाने के निमंत्रण का वचन दिया था। तब उसने (एडला) उसे बैठने और भोजन खाने के लिए कहा। शाम के समय क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया। उसने प्रत्येक का धन्यवाद किया।
अगली सुबह लोहार और उसकी बेटी क्रिसमस की सेवा के लिए चर्च गए। चूहेदानी बेचने वाला अभी भी सोया हुआ था। चर्च में लोहार और उसकी बेटी को यह जानकारी मिली कि एक वृद्ध किसान को चूहेदानियाँ बेचने वाले एक व्यक्ति ने लूट लिया है। इस समाचार ने एडला को उदास कर दिया। उसके पिता को भय था कि चूहेदानियाँ बेचने वाला उनकी अनुपस्थिति में उनके चाँदी के सारे चम्मच चुरा सकता है लेकिन नौकर ने उन्हें बताया कि फेरी वाला अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। बल्कि वह लड़की के लिए एक छोटा पैकेट छोड़ गया है। पैकेट में उसे एक छोटी चूहेदानी मिली। पैकेट के अंदर दस-दस क्रॉनर के तीन नोट थे और एक पत्र था। अपने पत्र में उसने उसके प्रति दयालुता दिखाने के लिए उसका धन्यवाद किया जैसे कि वह एक सचमुच का कैप्टन था। वह नहीं चाहता था कि क्रिसमस के अवसर पर उसको एक चोर के साथ रहने से कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। उसने लड़की से प्रार्थना की कि वह इस धन को वृद्ध किसान को लौटा दे। उसने लिखा कि चूहेदानी उसके लिए क्रिसमस का उपहार है।)
The Rattrap Word Meanings
[Page 32] :
Universal (belonging to the whole world) = सर्वव्यापक;
awakened (made mentally alive)= जागृत हुआ;
amidst (in the middle of) के बीच में;
legends (myths) पौराणिक बातें;
rattrap (device for catching rats) =चूहेदानी;
odd(notregular)=अनियमित;
especially(particularly) विशेषतौर पर;
profitable(giving profits)=फायदेमंद;
resort to (forced to do) = करने पर मजबूर होना;
petty (small) = छोटा, तुच्छ;
thievery (stealing) = चोरी;
rags (old, torn clothes) = चिथड़े;
sunken (hollow) = पिचकी हुई;
gleamed (shone) = चमकना;
monotonous (boring, joyless)= नीरस;
vagabond(wanderer )= आवारा;
plod (trudge)= कठिनाई से चलना;
meditation (deep thinking) = मनन;
struck (suddenly came to mind) = मन में विचार आना।
[Page 33] :
Existed (lived, remained) = जीवित रहना;
set bait (place food, etc to catch an animal) = चारा/फांस;
shelter(refuge) = शरण;
pork (pig meat)= सूअर का मांस;
tempted (lured)= प्रलोभित करना;
unwonted (not habitual) = आदत न होना;
cherished (held dear) = प्रिय;
pastime (means of entertainment) = मनोरंजन का साधन;
dreary (dull) = नीरस;
snare (trap) = जाल;
trudging (wandering) = आवारागर्दी;
sour (unpleasant) = अप्रिय;
porridge (oat meal) = दलिया;
carved off (cut)= काटा;
mjolis (a game of cards) = ताश का खेल;
prosperity (affluence) = समृद्धि;
crofter (who farms a piece of land) = छोटा किसान;
supported (sustained) = सहारा;
creamery (a small dairy)= छोटी डेयरी;
kronor (swedish currency) = स्वीडन की मुद्रा;
incredulous (unbelievable) = अविश्वसनीय;
bossy (domineering) = रौबीला;
pouch (small bag) = छोटी थैली;
nodding (shaking head) = सिर हिलाना।

[Page 34] :
Stuffed (packed tightly)= ठूसना;
in good season (cheerfully) = खुशी से;
peddler (travelling vendor)= फेरी वाला;
smashed (broke) = तोड़ा;
pane (window glass)= खिड़की का शीशा;
thrust (pushed) = डाले;
got hold (caught)=पकड़े;
smartness (cleverness)=चालाकी;
confusing(perplexing)= परेशान करने वाली;
fooled (deceived) = धोखा दिया;
bait(food to lure and catch animal)=फाँसने का सामान;
trunks(stems)=तने;
thickets(bushes)=झाड़ियाँ।
[Page 35]:
Descending (coming down) = नीचे आते हुए;
gloom (sadness) = उदासी;
despair (disappointment) = निराशा;
sank down (sat down) = बैठ गया;
staggered (walked unsteadily) = लड़खड़ाया;
summoned (gathered collected) = इकट्ठा किया;
smelter (one who melts ore to get metal from it) = धातु गलाने वाले;
forge (furnace) = भट्ठी;
barges (boats)= किश्तियाँ;
scow (flat bottomed boat)= चपटे तले वाली नाव;
dripping (thoroughly wet)= पुरी तरह से गीला;
groaned (moaned) =कराहना;
sifted (separated) = अलग;
pig iron (raw iron)=कच्चा लोहा;
anvil(an iron block on which a blacksmith hammers things) = निहाई;
glowing (shining) = चमकना;
stir (move a little) = कुछ हिलना;
bellows (device for producing a strong blast of air) = धौंकनी;
hovelled (put through shovels) = फावड़े से डालना;
clatter (loud noise) = जोर की आवाज;
whipped (sharp blowing or thrusting)= चाबुक मारना;
unusual(uncommon)=असाधारण;
vagabonds (wanderers) = आवारा;
sooty (covered with soot) = कालिख भरा।
[Page 36]:
Glanced (looked at)=देखा;
casually (carelessly)= लापरवाही से;
indifferently (without caring) = बिना परवाह किए;
intruder (one who is not invited) = घुसपैठिया;
ragged (shabbily clothed) = फटेहाल;
haughty (proud) = घमण्डी;
consent (agreement) = रजामन्दी;
tramp (wanderer) = आवारा;
ship out(shape out)= आकृति बनाना;
prominent (famous) = प्रसिद्ध;
ragamuffin (wearing rags) = फटेहाल;
eased(relaxed)=ढीला किया;
deigned(bothered) = तंग किया;
slouche(crouches)=दुबकना;
acquaintance (known, farniliar with) =परिचित, मित्र;
manor(farmhouse) = फार्महाउस;
comrade (friend) = साथी।
[Page 37]:
Alarmed (frightened) = भयभीत;
voluntarily (willingly) = इच्छापूर्वक;
apprentice (trainee) = नौसिखिया;
den (cave) = गुफा;
sneak away (go away unnoticed) = चुपके से चले जाना;
inconspicuously (without being noticed) = बिना नजर आए;
assumed (supposed) = कल्पना की;
embarrassed (feeling uneasy) = असुविधा महसूस करना;
abroad (in a foreign country) = विदेश में;
give in (surrender) = हार मान लेना;
persuasion (bringing round) = मनाना
valet (servant)= नौकर;
modest (gentle)= विनम्र;
glowed (shone )= चमका।

[Page 38] :
Stretched (spread out)= फैला हुआ;
evidently (obviously)= प्रत्यक्ष रूप से;
abruptly (suddenly) = अचानक;
compassionately (sympathetically)= सहानुभूति से;
bother (worry)= चिन्ता;
astonished (surprised)= हैरान;
glance (look at) = देखना;
forebodings (predictions)= भविष्यवाणी;
probably (perhaps) = शायद।
[Page 39] :
Queer (strange) = अजीब;
fall away (go away) = चले जाना;
starched (stiffed) = सख्त;
puckered (wrinkled) =झुर्रियों वाला;
uncertain (not clear) = अस्पष्ट;
dissimulate(hide)= छिपाना;
splendour(grandeur)=शान;
sheriff (an officer for keeping law and order)= पुलिस अफसर;
struck (gave a blow)= प्रहार करना;
rind (peel) = छिला हुआ।
[Page 40]:
Christmassy (of Christmas)= क्रिसमस का;
wretch (unfortunate)=अभागा;
interceded (mediated) = बीच बचाव किया;
cross-examined (interrogated) = पूछताछ की;
mumbled (murmured) = बुड़बुड़ाया;
preach (sermonize)= उपदेश देना;
parson (priest) = पादरी;
regret (to repent) = पछताना।
[Page 41]:
Crazy (mad) पागल;
fare (festivity)=उत्सव का माहौल;
blinking (winking rapidly)=आँख झपकाना;
aroused (woken up)= जागृत हुआ;
intention (desire) = इच्छा;
boundless (endless)= अनन्त;
amazement(surprise) =हैरानी।
[Page 42] :
Dejectedly (sadly) = उदासी से;
done up (finished) = समाप्त;
contents (things, inside) = अन्दर की चीजें;
agged (rough) = खुरदरा।
The Rattrap Translation in Hindi
Once upon a time there was a man who went around selling small rattraps of wire. He made them himself at odd moments, from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes.
No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rattraps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him-the whole world with its lands and seas, its cities and villages-was nothing but a bit rattrap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rattrap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end.
(एक बार की बात है जब एक आदमी घूम-घूम कर तार से बनी छोटी-छोटी चूहेदानियाँ बेचा करता था। जो कुछ सामान उसे दुकानों और बड़े फार्मों पर माँगकर मिलता उससे वह स्वयं ही मुश्किल के समय उन्हें बनाया करता था। फिर भी यह धन्धा कोई विशेष फायदेमन्द नहीं था, और इसलिए भूखों मरने से बचने के लिए उसे भीख माँगने और छोटी-छोटी चोरी, दोनों का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी उसके शरीर पर चिथड़े थे, उसके गाल पिचके हुए थे और उसकी आँखों में भूख चमकती थी।
कोई यह सोच नहीं सकता कि ऐसे आवारा व्यक्ति के लिए जीवन कितना उदास और नीरस होगा जो अपने विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता हो। मगर एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसे विचारों में खो गया जो उसे सचमुच बड़े मनोरंजक लगे। स्वाभाविक तौर पर वह अपने चूहों के पिंजरों के बारे में सोच रहा था, जब अचानक उसे यह ख्याल आया कि उसके चारों ओर का सारा संसारदेशों और सागरों, शहरों और गाँवों सहित-एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनुष्यों को दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त इसके अस्तित्व का कभी कोई अन्य उद्देश्य ही न था। इसमें धन और खुशियाँ हैं, आश्रय और भोजन है, गर्मी और वस्त्र हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदानी में पनीर और सूअर का मांस होता है और जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को दानों को छूने के प्रलोभन में आने देता है, पिंजरा उसके लिए बन्द हो जाता है और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है।)
The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwonted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his, during many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait.
(संसार निःसन्देह उस पर कभी अधिक मेहरबान नहीं रहा था। इसलिए इसके बारे में बुरा सोचने में उसे असाधारण आनन्द आता था। अपनी अनेक पैदल यात्राओं में समय बिताने के लिए यह उसका प्रिय काम हो गया कि अपने परिचित व्यक्तियों में उनके बारे में सोचे जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक पिंजरे में फंसने दिया था और उन अन्य व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी दाने (ललचाने वाली वस्तु) के चारों तरफ घूम रहे थे।)
One dark evening as he was trudging along the road he caught sight of a little gray cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper; then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger’s pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played ‘mjölis’ with his guest until bedtime.

(एक अन्धेरी शाम जब वह सड़क पर चला जा रहा था, तब उसने सड़क के किनारे बने सलेटी रंग के एक छोटे से मकान को देखा और रात के लिए आश्रय माँगने के लिए उसने वह दरवाजा खटखटाया। उसे इनकार भी नहीं किया गया। आमतौर पर जो रूखे चेहरे उसे मिला करते थे उनके स्थान पर वह बिना पत्नी और बच्चे वाला बूढ़ा मालिक अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर खुश हुआ। उसने तुरन्त दलिए के बर्तन को आग पर चढ़ा दिया और उसे रात्रि का भोजन दिया और फिर उसने अपनी तम्बाकू की रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो उसके और अजनबी दोनों की चिलम के लिए काफी था। अन्त में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ ताश खेलता रहा।)
The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjö Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labour, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of thirty kronor in payment.
(वह बूढ़ा व्यक्ति अपने मन की बात बताने में किसी पर भरोसा करने में उतना ही उदार था जितना कि दलिया व तम्बाकू देने में। उसने अपने अतिथि को तुरन्त बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रेमस्जो लौह मिल में काम करता था और खेती भी करता था। अब वह मजदूरी नहीं कर सकता, तो उसका गाय से गुजारा चलता है। हाँ, वह बहुत असाधारण है। वह प्रतिदिन डेरी के लिए दूध देती है और पिछले मास उसे भुगतान में तीस क्रॉनर मिले थे।)
The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled ten-kronor bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch.
(ऐसा लगा होगा कि अजनबी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया, एक चमड़े की थैली उतारी जो इस खिड़की में लगी एक कील से लटकी हुई थी और इसमें से दस क्रॉनर के तीन मुड़े हुए नोट निकाले। ये तीनों उसने मेहमान की आँखों के सामने रखे, जान-बूझकर सिर हिलाते हुए और वापिस उनको थैली में रख दिया।)
The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rattraps said good bye and thank you, and thereupon each went his own way.
(अगले दिन दोनों व्यक्ति प्रसन्नता से उठे। किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था, और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे लेटे नहीं रहना चाहिए। दोनों ने ही घर को एक-साथ छोड़ा। किसान ने ताला बन्द किया और चाबी अपनी जेब में डाली। चूहेदानियों वाले आदमी ने उसको अलविदा कहा और धन्यवाद किया, और इसके बाद दोनों अपने-अपने रास्ते चल दिए।)
But half an hour later the rattrap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the thirty kronor. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away.
(मगर आधे घण्टे बाद चूहेदानी बेचने वाला आदमी फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने अन्दर जाने की कोशिश नहीं की। वह केवल खिड़की तक गया, एक शीशे को तोड़ा, अपने एक हाथ को अन्दर डाला और तीस क्रॉनर वाली थैली को अपने हाथ में पकड़ा। उसने पैसे निकाले और इन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने चमड़े की थैली को वापिस बड़ी सावधानी से इसकी जगह पर रख दिया और चला गया।)
As he walked along with the money in his pocket he felt quite pleased with his smartness. He realised, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road, into the woods. During the first hours this caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into.
He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely! He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realised that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rattrap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape.
(अपनी जेब में पैसे डालकर जब वह जा रहा था, उसे अपनी चालाकी पर बड़ी खुशी हुई। निःसन्देह उसने यह अनुभव भी किया कि अब वह सामान्य सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मगर उसे सड़क से मुड़कर जंगल में चलना चाहिए था। पहले कुछ घण्टों में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। बाद में दिन के अन्तिम भाग में हालात बिगड़ गए; क्योंकि जिस जंगल में वह प्रवेश कर चुका था वह बड़ा और चक्कर में डालने वाला था।
उसने प्रयत्न किया कि वह निश्चयपूर्वक एक निश्चित दिशा में चले परन्तु रास्ते ऐसे विचित्र ढंग से आगे-पीछे मुड़ जाते थे। वह चलता ही गया और जंगल का कोई अन्त ही नहीं होता था और अन्ततः उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के एक ही भाग में चक्कर काट रहा था। फौरन उसे अपने संसार और चूहेदानी के बारे में किए गए विचारों का ध्यान आया। अब उसकी बारी आ गई थी। उसने अपने-आपको दाने के लालच में मूर्ख बनने दिया था और पकड़ा गया था। सारे जंगल ने अपने वृक्षों और शाखाओं, तनों और गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों से उसे घेर लिया था मानो कि वह एक अभेद्य जेल हो जिससे अब वह निकल नहीं सकता था।)
It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger, and increased also his gloom and despair. Finally he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. “Those are the hammer strokes from an iron mill”, he thought. “There must be people near by”. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound.
(दिसम्बर के अन्तिम दिन थे। अन्धकार पहले ही जंगल में आने लगा था। इस बात ने खतरे को और बढ़ा दिया, और उसकी उदासी और निराशा को भी। अन्त में बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं नजर नहीं आया और थकान के कारण मुर्दा-सा वह जमीन पर ही बैठ गया। पर जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी-एक कठोर लगातार ठक-ठक की आवाज। इसमें कोई शक नहीं था कि वह क्या थी। वह उठ खड़ा हुआ। “यह लोहे के कारखाने से आती हुई हथौड़े के चोटों की आवाज है”, उसने सोचा। “लोग पास ही होने चाहिएँ” उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ आवाज की दिशा में चल पड़ा।)
The Ramsjö Ironworks, which are now closed down, were, not so long ago, a large plant, with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates.
(रमस्जो लौह मिल, जो अब बन्द हो चुका है कुछ समय पहले तक एक बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलाने का यन्त्र, रोलिंग मिल और भट्ठी थी। गर्मी के दिनों में पूरे भरे छोटे जहाज और नौकाएँ नहर में उतारी जाती थीं जो एक बड़ी झील में जाती थीं और सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़कें उस कोयले से काली रहती थीं जो चारकोल की बड़ी-बड़ी क्रेटों से झरता रहता था।)
During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes.
(क्रिसमस के पहले की एक लम्बी अन्धेरी शाम को मुख्य लोहार और उसके सहयोगी अन्धेरी भट्ठी में चूल्हे के पास बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भट्ठी पर चढ़ा हुआ कच्चा लोहा इस लायक हो जाए कि उसे निहाई पर रखा जा सके। थोड़ी देर में उनमें से एक व्यक्ति उठता, एक लम्बी लोहे की छड़ी से उस लोहे को चलाता और पसीने से तर होकर कुछ क्षणों में वापस आ जाता, यद्यपि परम्परा के अनुसार वह व्यक्ति एक लम्बी कमीज और काठ के जूतों के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनता था।)
All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shovelled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge, until he stood close up to the furnace.
(हर समय भट्ठी में तरह-तरह की आवाजें सुनाई देती थीं। बड़ी-बड़ी धौंकनियाँ कराहने की आवाज करती और जलता हुआ कोयला चटकता रहता। आग पर काम करने वाला लड़का फावड़े से उठाकर कोयला भट्ठी में डालता था और जोर की आवाज होती थी। बाहर झरने की तेज आवाज होती थी और तेज उत्तरी हवा ईंटों, टाइलों की बनी छत पर बरसात को कोड़े की तरह पटकती थी। शायद इस सारे शोर के कारण लोहार ने यह तब तक नहीं देखा कि कोई आदमी गेट खोलकर भट्ठी के अन्दर आ गया है जब तक कि वह चूल्हे के बिल्कुल पास ही नहीं आ गया।)

Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in fornt of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rattraps dangling on his chest.
He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honouring him with a single word. The tramp did not say anything, either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep.
(अवश्य ही, रात बिताने के लिए आश्रयहीन रहने वाले घुमक्कड़ों का रोशनी की चमक के पास भट्ठी की तरफ आकर्षित होना, जो रोशनी काली खिड़कियों में से आती थी, और उनका अपने-आपको गर्म करने के लिए आग के सामने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। लोहारों ने बाहर से आने वाले आदमी की तरफ सहजता और उदासीनता से देखा। वह इस तरह दिखता था जैसे उसके तरह के लोग प्रायः दिखते थे, लम्बी, धूल भरी, खुरदरी दाढ़ी और चूहेदानियों का एक गुच्छा उसकी छाती पर लटकता हुआ। उसने वहाँ रुकने की आज्ञा माँगी, और मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर, उसको एक शब्द भी सम्मान का कहे बिना घमण्ड से भरी हुई सहमति दे दी।
उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। वह वहाँ बातें करने के लिए नहीं, बल्कि अपने-आपको गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था।)
In those days the Ramsjö iron mill was owned by a very prominent ironmaster, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection.
(उन दिनों रेमस्जो लौह मिल का मालिक एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था जिसका महानतम उद्देश्य अच्छा लोहा जहाजों में भरकर बाजार में भेजना था। वह रात-दिन देखता था कि काम जितना सम्भव हो सके उतना अच्छी तरह से हो, और ठीक उसी समय वह भट्ठी में रात के समय का निरीक्षण करने आया था।)
Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. “But of course, it is you, Nils Olof!” he said. “How you do look !”
(निःसन्देह जो चीज उसने सबसे पहले देखी वह था वह चिथड़े पहने हुए लम्बा आदमी जो आराम पाने के लिए भट्ठी के इतना पास आ गया था कि उसके चिथड़ों से भाप उठ रही थी। आयरन मास्टर ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने अजनबी की तरफ देखा भी नहीं था। वह उसके करीब आया, उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए अपनी तिरछी टोपी को उतारा। “परन्तु अवश्य तुम हो, नील्स ऑलोफ!” उसने कहा। “तुम कैसे दिखते हो!”)
The man with the rattraps had never before seen the ironmaster at Ramsjö and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor. Therefore he did not want to undeceive him all at once. “Yes, God knows things have gone downhill with me”, he said.
(चूहेदानी वाले व्यक्ति ने रेमस्जो के आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। परन्तु उसे लगा कि अगर वह श्रेष्ठ भद्रपुरुष उसे कोई पुराना परिचित समझता है तो वह शायद उसको दो क्रॉनर दे दे। अतः वह तुरन्त ही उसका धोखा दूर करना नहीं चाहता था। “हाँ, भगवान् जानता है, मेरे साथ बुरा हुआ है,” वह बोला।)
“You should not have resigned from the regiment”, said the ironmaster. “That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me.” To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental corade-that, however, did not please the tramp.
(“तुम्हें फौज से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था,” आयरन मास्टर बोला। “वह गलती थी। अगर मैं उस समय तक फौज में होता, तो ऐसा कभी न होता। खैर, अब निःसन्देह, तुम मेरे साथ घर चलोगे।”
बड़े फार्म हाउस पर जाना और मालिक के द्वारा एक पुराने फौजी साथी की तरह स्वागत किया जाना इस बात से तो वह घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ।)
“No, I couldn’t think of it !” he said, looking quite alarmed. He thought of the thirty kronor. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion’s den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing.
(“नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता।” वह एकदम डरकर बोला। उसने तीस क्रॉनर के बारे में सोचा। फार्म हाउस तक जाने का अर्थ था कि जान-बूझकर शेर की मांद में जाना। वह तो सिर्फ लोहे की मिल मे सोना चाहता था और तब जहाँ तक सम्भव हो बिना किसी के पता लगे चुपचाप खिसक जाना। आयरन मास्टर को लगा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदगी अनुभव कर रहा है।)
“Please don’t think that I have such a fine home that you cannot show yourself there”. He said… “Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn’t have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster.”
(“कृपया आप ऐसा न सोचें कि मेरा घर इतना बढ़िया है कि आप उसमें नहीं जा सकते।” वह बोला, “एलिजाबेथ मर चुकी है, आपको पहले यह पता चल चुका होगा। मेरे लड़के विदेश में हैं। और घर पर मेरी बड़ी बेटी और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे पास कोई साथी नहीं है। अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस का भोजन थोड़ा शीघ्र समाप्त करने में हमारी सहायता करो।”)

But the stranger said no, and no, and again no, and the ironmaster saw that he must give in. “It looks as though Captain Von Stahle preferred to stay with you tonight, Stjernström”, he said to the master blacksmith and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself.
(परन्तु अजनबी ने बार-बार ना कहा, और आयरन मास्टर को लगा उसे हार माननी पड़ेगी। “ऐसा लगता है मानो कप्तान वॉन स्टाल आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहेगा, स्टेर्नस्टोर्म”, उसने मुख्य लोहार को कहा और मुड़ा। परन्तु वह जाते हुए खुद ही अपने-आप में हँसा, और लोहार, जो उसको जानता था, भली प्रकार समझ गया कि उसने अपने अन्तिम शब्द नहीं कहे थे। आधा घण्टे से अधिक नहीं बीता होगा कि उन्हें भट्ठी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी और एक नया मेहमान अन्दर आया, पर इस बार आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था, लगता था कि उसे उम्मीद थी कि उसकी अपेक्षा उस (बेटी) में मनाने की शक्ति अधिक है।)
She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened.
(वह आई, उसके पीछे-पीछे एक बड़ा फर वाला कोट हाथ में लिए एक नौकर था। वह सुन्दर बिल्कुल न थी पर वह विनम्र और काफी शर्मीली लगती थी। लौह मिल में हर वस्तु वैसी ही थी जैसी कि शाम के प्रारम्भ में थी। मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी अपने बैंच पर बैठे थे और लोहा और कोयला चूल्हे में अभी भी दहक रहे थे। अजनबी फर्श पर लेट गया था और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लिया और उसने अपना टोप अपनी आँखों पर डाल लिया था। युवा लड़की की जैसे ही उस पर नजर पड़ी, वह उसके पास गई और उसका टोप उठाया। साफ तौर पर उस आदमी को खुली आँखों से सोने की आदत थी। वह एकदम उछल पड़ा और लगता था कि काफी डर गया था।)
“My name is Edla Willmansson,” said the young girl. “My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time.”
(“मेरा नाम एडला विलमनसन है,” युवा लड़की ने कहा। “मेरे पिता ने घर आकर बताया कि आप आज रात यहाँ लौह मिल में सोना चाहते हो और तब मैंने यहाँ आने की और आपको अपने घर ले जाने की आज्ञा माँगी। कैप्टन, मुझे बड़ा दुःख है कि आप इतनी मुश्किल हालत में हो।”)

She looked at him compassionately, with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. “Either he has stolen something or else he has escaped from, jail”, she thought, and added quickly, “You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve.”
(उसने उसकी भारी आँखों से उसको करुणापूर्वक देखा, और तब उसने देखा कि वह आदमी डर गया है। “या तो उसने कुछ चुराया है या वह जेल से निकलकर भागा है,” उसने सोचा और जल्दी ही कहा, “आप निश्चित हो सकते हैं, कप्तान, कि जितनी आसानी से आप हमारे पास आए हैं उतनी आसानी से ही आपको जाने दिया जाएगा। बस हमारे साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ठहरें।”)
She said this in such a friendly manner that the rattrap peddler must have felt confident in her. “It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss,” he said. “I will come at once.” He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmiths so much as a glance.
(उसने यह बात इतनी मित्रतापूर्वक कही कि चूहेदानी बेचने वाले को उसमें विश्वास महसूस हुआ। “मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरे लिए अपने-आपको तकलीफ दोगी, मिस,” उसने कहा। “मैं तुरन्त तुम्हारे साथ चलूँगा।”
उसने फर कोट, जो नौकर ने उसको दिया उसे झुककर स्वीकार किया, इसको अपने फटे कपड़ों पर डाला और हैरान लोहारों पर बिना दृष्टि डाले युवा लड़की के पीछे बाहर खड़ी-खड़ी गाड़ी तक गया।)
But while he was riding up to the manor house he had evil forebodings. “Why the devil did I take that fellow’s money?” he thought. “Now I am sitting in the trap and will never get out of it.” The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly.
(परन्तु जब वह फार्म हाउस जा रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। “मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए?” उसने सोचा। “अब मैं जाल में फंस गया हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकूँगा।” अगले दिन क्रिसमस था और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आया तो शायद उसने सन्तुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा जिसको वह इतना अचानक मिल गया था।)
“First of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones,” he said to his daughter, who was busy at the table. “And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rattraps.” “It is queer that things have gone downhill with him as badly as that,” said the daughter.” “Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man.”
(“सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा माँस आए”, उसने अपनी लड़की से कहा, जो टेबल पर व्यस्त थी। “और तब हमें यह देखना होगा कि वह पास घूम-घूम कर चूहेदानी बेचने की बजाय करने के लिए कोई अन्य काम करे।” “यह अजीब है कि उनके साथ बुरा हुआ”, लड़की ने कहा। “कल रात को मैं नहीं सोचती थी कि उसके पास यह दिखाने के लिए कुछ था कि वह कभी भी एक शिक्षित आदमी रहा है।”)
“You must have patience, my little girl,” said the father. “As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes.”
Just as he said this the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a starched collar and white shoes.
(“मेरी प्रिय बेटी, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए,” पिता ने कहा । “जैसे ही साफ-सुथरा होगा और ढंग से कपड़े पहनेगा, तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। पिछली रात वह, स्वाभाविक था कि शर्मिंदा था। आवारा कपड़ों के साथ ही उसके आवारा तौर-तरीके भी चले जाएँगे।” जैसे ही उसने यह कहा कि दरवाजा खुला और अजनबी अन्दर आया। हाँ, अब वह वाकई साफ-सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने था। नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे थे और शेव की थी। इसके अतिरिक्त वह आयरन मास्टर का सुन्दर सूट पहने था। वह एक सफेद कमीज और कलफ लगा कालर तथा सफेद जूते पहने था।)
But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. “What does this mean?” he thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendour had come to an end.
(लेकिन यद्यपि यह मेहमान अब सजा संवरा था, आयरन मास्टर खुश नजर नहीं आया। उसने माथे पर त्योंरी डालकर उसे देखा, और यह समझना आसान था कि जब उसने अजनबी को भट्ठी की हल्की रोशनी में देखा था, शायद उससे गलती हो गई थी, परन्तु अब जबकि दिन के खुले प्रकाश में वह उसके सामने खड़ा था, उसे, भ्रमित होकर कोई पुराना मित्र समझना असम्भव था। “इसका क्या अभिप्राय है?” वह दहाड़ा। “अजनबी ने कुछ और दिखाने की कोशिश करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने तुरन्त ही भाँप लिया कि शानो-शौकत का अन्त आ गया है।)
“It is not my fault, sir,” he said. “I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away.” “Well,” said the ironmaster, hesitating a little, “it was not quite honest, either. You must admit that, and I should not be surprised it the sheriff would like to have something to say in the matter.”
(“श्रीमान, यह मेरी गलती नहीं है,” वह बोला, “मैंने कभी भी एक गरीब फेरी वाला होने के अतिरिक्त कोई और दिखावा नहीं किया, और मैंने तर्क दिया और प्रार्थना की कि मुझे लौह मिल पर ही रहने दिया जाए। पर कोई हानि नहीं हुई है। मैं फिर से अपने चिथड़े पहनकर जा सकता हूँ।” “खैर,” आयरन मास्टर कुछ झिझक के साथ बोला, “पर यह बात पूरी ईमानदारी वाली नहीं थी। यह बात तुम्हें माननी होगी, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर शेरिफ इस विषय में कुछ कहना चाहें।”)

The tramp took a step forward and struck the table with his fist. “Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are,” he said. “This whole world is nothing but a big rattarp. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap.” The ironmaster began to laugh.
(उस आवारा व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेज पर मुक्का मारा। “अब मैं आपको बताता हूँ, श्री आयरन मास्टर, कि क्या बात है,” वह बोला । “यह सारा संसार एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपके सामने जो भी अच्छी वस्तुएँ प्रस्तुत होती हैं वे पनीर के छिलके और सूअर का माँस के टुकड़ें के अलावा कुछ नहीं है जिन्हें किसी लाचार व्यक्ति को मुसीबत में खींचने के लिए लगाया गया है। और अब अगर शेरिफ आता है और मुझे इस बात के लिए कैद कर देता है तो आयरन मास्टर आप इतना अवश्य याद रखें कि ऐसा दिन भी आ सकता है कि जब आप खुद पोर्क का कोई बड़ा टुकड़ा पाना चाहों और तब आप जाल में फँस जाओ।”
आयरन मास्टर हँसने लगा।)
“That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can.”
But just as the man was opening the door, the daughter said, “I think he ought to stay with us today. I don’t want him to go.” And with that she went and closed the door.
“What in the world are you doing?” said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought now homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond.
(“भले व्यक्ति, यह बात कोई बुरी तरह से नहीं कही गई। शायद क्रिसमस की पूर्व-संध्या पर हम शेरिफ को रहने ही दें। लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ।” लेकिन जब वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, बेटी बोली, “मेरे ख्याल से आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए।” और इसके साथ ही उसने दरवाजा बन्द कर दिया।
“तुम यह भला क्या कर रही हो?” पिता ने कहा।
पुत्री बड़ी शर्मिंदा होकर वहाँ खड़ी रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। उस प्रातः वह बड़ी खुश यह सोचकर हो रही थी कि वह गरीब भूखे अभागे व्यक्ति के लिए कैसी घर जैसी और क्रिसमस जैसी व्यवस्था करने जा रही थी। वह इस विचार को एकदम नहीं त्याग सकती थी और यही कारण था कि उसने उस आवारा का पक्ष लिया।)
“I am thinking of this stranger here,” said the young girl. “He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here-just one in the whole year.”
(“मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ,” युवा लड़की ने कहा। “सारे साल यह चलता ही रहता है और शायद पूरे देश में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वह चैन से रह सके। जिधर भी वह जाता है, उसे भगा दिया जाता है। उसे सदा गिरफ्तार होने और सवाल पूछे जाने का डर सताता रहता है। मैं चाहूँगी कि वह यहाँ हमारे साथ एक दिन शान्ति का गुजार ले-पूरे साल में केवल एक दिन।”)
The ironmaster mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. “It was all a mistake, of course,” she continued. “But anyway I don’t think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, and to whom we have promised Christmas cheer.” “You do preach worse than a parson,” said the ironmaster. “I only hope you won’t have to regret this.”
(आयरन मास्टर धीरे से कुछ बड़बड़ाया। वह उसका विरोध नहीं कर सका। “माना कि यह सब एक गलती थी,” वह बोलती गई। “पर फिर भी मैं नहीं सोचती कि हमें ऐसे एक आदमी को भगा देना चाहिए जिससे हमने यहाँ आने के लिए कहा और जिसे हमने क्रिसमस की खुशी देने का वायदा किया।” “तुम तो पादरी से भी अधिक बुरा उपदेश देती हो,” आयरन मास्टर बोला। “मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि तुम्हें इस बात के लिए पछताना न पड़े।”)
The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. “Now sit down and eat,” she said, for she could see that her father had given in. The man with the rattraps said not a word; he only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be?
(युवा लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गई। “अब बैठ जाओ और खाओ,” वह बोली, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली थी।
चूहेदानी वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वह बोला, वह केवल बैठ गया और खाना खाता रहा। समय-समय पर वह उस युवा लड़की को देख लेता था जिसने उसका पक्ष लिया था। उसने ऐसा क्यों किया था ? इसके पीछे क्या पागलपन भरा विचार हो सकता था ?)
After that, Christmas Eve at Ramsjö passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo.

(इसके बाद क्रिसमस की पूर्व-संध्या रेमस्जो में वैसे ही गुजरी जैसी यह सदा गुजरा करती थी। अजनबी किसी परेशानी का कारण नहीं बना क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं। दोपहर बाद वह एक गेस्ट रूम के सोफे पर पड़ा लगातार सोता रहा। दोपहर में उन्होंने उसे क्रिसमस के अच्छे भोजन में अपना हिस्सा लेने के लिए जगाया, पर उसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लगता था कि बहुत वर्षों से वह इतनी शान्ति और सुरक्षा से नहीं सोया था जैसी कि यहाँ रेमस्जो में उसे मिली थी।)
In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. Two hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge.
(शाम को जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया तो उन्होंने उसको दुबारा जगाया, और वह थोड़ी देर तक ड्राईंग रूम में इस तरह पलक झपकता हुआ खड़ा रहा मानो मोमबत्ती की रोशनी उसे चुभ रही हो, परन्तु इसके बाद वह दुबारा सोने चला गया। दो घण्टे बाद उसे एक बार फिर जगाया गया। इस बार उसे नीचे डाईनिंग रूम में जाना पड़ा और क्रिसमस के उपलक्ष्य में मछली और दलिया खाया।)
As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night, but when he came to the young girl she gave him to understand that it was her father’s intention that the suit which he wore was to be a Christmas present-he did not have to return it; and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. The man with the rattraps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement.
(ज्योंहि वे टेबल से खड़े हुए वह वहाँ उपस्थित हर एक के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा, परन्तु जब वह जवान लड़की के पास आया उसने उसे समझाया कि जो सूट वह पहने हुए है वह उसके पिता की तरफ से उसको क्रिसमस का उपहार है उसे उसको लौटाने की जरूरत नहीं है; और यदि वह अगले वर्ष क्रिसमस एक ऐसी जगह बिताना चाहे जहाँ वह शान्ति से रहे और निश्चित हो कि जहाँ उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो उसका यहाँ पर फिर से स्वागत होगा। चूहेदानी वाले आदमी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल लड़की की तरफ असीमित हैरानी में देखा।)
The next morning the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep, and they did not distrub him. When, at about ten o’clock, they drove back from church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rattraps. “Yes, that was a fine fellow you let into the house,” said her father. “I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard this time.”
(अगली प्रातः को आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस की धार्मिक रस्म को करवाने के लिए जल्दी जाग गए। उनका मेहमान अभी सोया हुआ था और उन्होंने उसे नहीं जगाया। जब लगभग दस बजे वे चर्च से लौटे, तो युवती पहले से अधिक उदासी से सिर नीचा करके बैठ गई। चर्च में उसे पता चला था कि एक बूढ़े किसान को एक घूम-घूम कर चूहेदानियाँ बेचने वाला आदमी लूटकर चला गया। “हाँ, वह बढ़िया आदमी था जिसे तुमने घर में रहने दिया था”, उसके पिता ने कहा, “मैं नहीं समझता कि अब तक घर की अलमारी में कोई चाँदी का चम्मच बचा होगा।”)
The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Willmansson was to be kind enough to accept as a Christmas present.
(गाड़ी सामने की सीढ़ियों के आगे मुश्किल से रुकी होगी जब आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी वहीं है। उसने यह भी कहा कि वह चर्च में सुनकर आया है कि वह आदमी चोर है। नौकर ने उत्तर दिया कि वह आदमी जा चुका और वह अपने साथ कोई चीज नहीं ले गया है। इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा-सा पैकेट छोड़ गया है जिसे मिस विलमनसन कृपया एक क्रिसमस की भेंट समझ स्वीकार करें।)
The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rattrap, and in it lay three wrinkled ten kronor notes. But that was not all. In the rattrap lay also a letter written in large, jagged characters
(युवा लड़की ने पैकेट खोला जो इतनी बुरी तरह लपेटा गया था कि उसके अन्दर का सामान तुरन्त ही नजर आ गया। खुशी की एक छोटी-सी चीख उसके मुँह से निकल गई। उसे एक छोटी-सी चूहेदानी मिली और इसमें 10 क्रॉनर वाले तीन नोट मुड़े हुए रखे थे। परन्तु इतना ही नहीं था। चूहेदान के अन्दर बड़े-बड़े टूटे-फूटे अक्षरों में लिखा एक पत्र भी था।)
“Honoured and noble Miss, “Since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you, in return, as if I was a real captain-for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a theif; but you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers.
(“सम्मानीय और श्रेष्ठ मिस साहिबा, “क्योंकि आपने सारा दिन मुझसे ऐसा अच्छा व्यवहार किया है जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूँ, बदले में मैं आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं असली कैप्टन ही हूँ; क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आपको किसी चोर के द्वारा शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि आप यह धन सड़क के किनारे रहने वाले बूढ़े व्यक्ति को दे देना जिसके धन की थैली गरीब आवारा लोगों को ललचाने के लिए दाने की तरह खिड़की की चौखट से लटकी रहती है।”)
‘
“The rattrap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world’s rattrap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. “Written with friendship and high regard, “Captain von Stahle.” (“यह चूहेदानी उस चूहे की ओर से एक क्रिसमस उपहार है जो इस संसार के चूहेदान में फंस गया होता अगर आपने कैप्टन न बनाया होता क्योंकि इसके कारण उसके अन्दर स्वयं को शुद्ध करने की शक्ति आ गई।” “मैत्रीभाव से और बड़े सम्मान से लिखा गया, “कैप्टन वॉन स्टाहल।”)
![]()
![]()
![]()